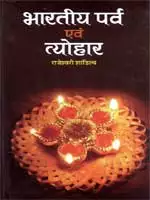|
धर्म एवं दर्शन >> भारतीय पर्व एवं त्योहार भारतीय पर्व एवं त्योहारराजेश्वरी शांडिल्य
|
206 पाठक हैं |
|||||||
भारतीय पर्व एवं त्योहारों का वर्णन
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भारत अनेकता में एकता का देश है। इसमें दुनिया के प्रायः सभी धर्म एवं
सम्प्रदाय मौजूद हैं, जिन्हें हर तरह की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और
वे अपने-अपने पर्व-त्योहार अपनी परंपरा के अनुसार मनाने के लिए स्वतंत्र
हैं। हमारे पर्व या त्योहार मात्र उत्सव नहीं होते जिन्हें उल्लास और उमंग
के साथ मनाकर एक औपचारिकता पूरी कर दी जाती है, बल्कि अधिकांश पर्वों में
एक संस्कृति, एक इतिहास और एक परंपरा निहित है।
कुछ पर्व ऐसे हैं जो अनेक स्थानों पर कई दिनों तक उत्सव के रूप में मानए जाते हैं, जैसे—मैसूर का दशहरा, कुल्लू का दशहरा या तिरुपति उत्सव आदि। पर्व एवं त्यौहारों की जो अविभाज्य परिकल्पना हिंदुओं में है, वह अन्य पंथों व संप्रदायों में कदाचित् ही मिले। वास्तव में हमारी संस्कृति ही उत्सवप्रिय है। यह हमारे समृद्ध सांस्कृतिक जीवन एवं गहन आध्यात्मिक चिंतन का प्रतिबिंब है।
प्रस्तुत पुस्तक में विभिन्न पर्वों एवं त्योहारों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। यह अत्यंत सुगमता से विभिन्न पर्वों एवं त्योहारों से संबंधित महत्वपूर्ण संदर्भों व तथ्यों की जानकारी प्रदान करती है।
कुछ पर्व ऐसे हैं जो अनेक स्थानों पर कई दिनों तक उत्सव के रूप में मानए जाते हैं, जैसे—मैसूर का दशहरा, कुल्लू का दशहरा या तिरुपति उत्सव आदि। पर्व एवं त्यौहारों की जो अविभाज्य परिकल्पना हिंदुओं में है, वह अन्य पंथों व संप्रदायों में कदाचित् ही मिले। वास्तव में हमारी संस्कृति ही उत्सवप्रिय है। यह हमारे समृद्ध सांस्कृतिक जीवन एवं गहन आध्यात्मिक चिंतन का प्रतिबिंब है।
प्रस्तुत पुस्तक में विभिन्न पर्वों एवं त्योहारों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। यह अत्यंत सुगमता से विभिन्न पर्वों एवं त्योहारों से संबंधित महत्वपूर्ण संदर्भों व तथ्यों की जानकारी प्रदान करती है।
प्रशस्तिवाक्
वर्ण, आश्रम एवं पुरुषार्थ की त्रिवेणी से मंडित होने के कारण ही तीर्थराज
कल्प भारतवर्ष प्राक्तन युग में विश्वगुरु के पद पर अधिष्ठित रहा है। आज
इन पवित्र शब्दों के अर्थ राजनीतिक प्रपंच की कालिमा से उपल्पित होने के
कारण न केवल परिवर्तित हो गए हैं, प्रत्युत नवयुगीन भाष्यकारों की भ्रांत
व्याख्याओं के कारण राष्ट्र के योग-क्षेम को भी दूषित कर रहे हैं।
वैयक्तिक राग-द्वेष से ओत-प्रोत इन व्याख्याकारों को संभवतः यह ज्ञान नहीं
है कि इस राष्ट्र की सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान संपदा, सारा चिंतन, सारी
शाश्वत-चिरंतन स्थापनाएँ मानवीय नहीं, आर्षकोटिक हैं। मानवीय ज्ञान,
मानवीय चिंतन, मानवीय स्थापना—व्यक्ति, देश एवं काल की सीमा में
बँधे होते हैं, फलतः परिवर्तित समाज, देश एवं कालावधि में वे खंडित हो
जाते हैं, परंतु इसके विपरीत, आर्षज्ञान, आर्षचिंतन एवं आर्षस्थापना
शाश्वत होती है, त्रिकालाबाधित होती है।
वर्ण, आश्रम एवं पुरुषार्थ आदि भी मानवीय आविष्कार नहीं हैं। ये सभी आर्षचिंतन के प्रसव हैं। फलतः ये सभी तत्त्व सार्वदेशिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनिक हैं। संपूर्ण विश्व चार वर्णों में विभक्त है। कौन ऐसा राष्ट्र है, जो ज्ञान, शक्तिसंचय, संपत्ति तथा कृषिकर्म के अतिरिक्त किसी पाँचवें पक्ष पर केन्द्रित हो। विश्व के किसी भी राष्ट्र की कोई भी गतिविधि हो, इन्हीं चारों वर्णों में समाहित हो जाती है। अब एक व्यक्ति अपने सीमित जीवन में सबकुछ तो कर नहीं सकता। फलतः वह चारो वर्णों में से किसी एक का वरण करता है—व्रियतेऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धयर्थम् इति वर्णः। अर्थात् अभ्युदय (सांसारिक उन्नति) एवं निःश्रेयस (पारलौकिक कल्याण) की सिद्धि के लिए जिसका वरण किया जाए, वही वर्ण है। इस वर्ण से ही समाज में मनुष्य का प्रत्यभिज्ञान एवं मूल्यांकन संभव होता है। संभवतः इसी दृष्टि से आचार्य मल्लिनाथ किरातार्जुनीय महाकाव्य की सर्वकंषा टीका में लिखते हैं—वर्णः प्रशस्तिः।
प्राध्यापक (साधक, वैज्ञानिक, चिंतक) सैनिक, व्यापारी अथवा कृषक होना-प्रशस्ति (Excellence) ही तो है। समाज में हमारी पहचान इसी रूप में होती है। आर्षचिंतन में इन्हीं प्रशस्ति साधनों को ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कहा गया है। यह व्यवस्था सर्वथा निर्दोष एवं निरवद्य है। यदि इस व्यवस्था की चरितार्थता (Application) में कोई कमी है तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है, प्रत्युत उस व्यवस्था का व्यवस्थापक समाज दोषी है। समाज को ही आत्म-विश्लेषण करना चाहिए।
भारतीय वर्ण-व्यवस्था कम-से-कम महाभारत काल तक तो जन्माश्रित नहीं थी। योगेश्वर कृष्ण स्वयं कहते हैं—अर्जुन ! गुण एवं कर्म पर आश्रित चातुर्वर्ण्य मैंने ही (ऋषियों के माध्यम से) निर्मित किया है—
वर्ण, आश्रम एवं पुरुषार्थ आदि भी मानवीय आविष्कार नहीं हैं। ये सभी आर्षचिंतन के प्रसव हैं। फलतः ये सभी तत्त्व सार्वदेशिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनिक हैं। संपूर्ण विश्व चार वर्णों में विभक्त है। कौन ऐसा राष्ट्र है, जो ज्ञान, शक्तिसंचय, संपत्ति तथा कृषिकर्म के अतिरिक्त किसी पाँचवें पक्ष पर केन्द्रित हो। विश्व के किसी भी राष्ट्र की कोई भी गतिविधि हो, इन्हीं चारों वर्णों में समाहित हो जाती है। अब एक व्यक्ति अपने सीमित जीवन में सबकुछ तो कर नहीं सकता। फलतः वह चारो वर्णों में से किसी एक का वरण करता है—व्रियतेऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धयर्थम् इति वर्णः। अर्थात् अभ्युदय (सांसारिक उन्नति) एवं निःश्रेयस (पारलौकिक कल्याण) की सिद्धि के लिए जिसका वरण किया जाए, वही वर्ण है। इस वर्ण से ही समाज में मनुष्य का प्रत्यभिज्ञान एवं मूल्यांकन संभव होता है। संभवतः इसी दृष्टि से आचार्य मल्लिनाथ किरातार्जुनीय महाकाव्य की सर्वकंषा टीका में लिखते हैं—वर्णः प्रशस्तिः।
प्राध्यापक (साधक, वैज्ञानिक, चिंतक) सैनिक, व्यापारी अथवा कृषक होना-प्रशस्ति (Excellence) ही तो है। समाज में हमारी पहचान इसी रूप में होती है। आर्षचिंतन में इन्हीं प्रशस्ति साधनों को ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कहा गया है। यह व्यवस्था सर्वथा निर्दोष एवं निरवद्य है। यदि इस व्यवस्था की चरितार्थता (Application) में कोई कमी है तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है, प्रत्युत उस व्यवस्था का व्यवस्थापक समाज दोषी है। समाज को ही आत्म-विश्लेषण करना चाहिए।
भारतीय वर्ण-व्यवस्था कम-से-कम महाभारत काल तक तो जन्माश्रित नहीं थी। योगेश्वर कृष्ण स्वयं कहते हैं—अर्जुन ! गुण एवं कर्म पर आश्रित चातुर्वर्ण्य मैंने ही (ऋषियों के माध्यम से) निर्मित किया है—
चातुर्यवर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।
वर्णानुसारी मानव जीवन चार आश्रमों में विभक्त हैं—ब्रह्मचर्य,
गार्हस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास। इन्हीं चार कालखंडों में मनुष्य जीवन के
चार पुरुषार्थ-अर्थ, काम, धर्म एवं मोक्ष—की सिद्धि में
प्रवृत्त
होता है। हमारा आर्षचिंतन मानव जीवन का विस्तार सौ वर्षों का मानवता
है—जीवेम शरदः शतम् (ऋग्वेद), अतः जीवन का प्रत्येक आश्रम
पच्चीस
वर्षों में सीमित है। इनमें प्रथम दो आश्रम तो प्रवृत्ति (भोग) परक हैं
तथा अन्य दो निवृत्ति (त्याग) परक। वर्ण एवं आश्रम के परिपालन में
पर्यवसित यही धर्म वर्णाश्रम धर्म में कहा गया है।
अर्थ्यते काम्यत इत्यर्थः। पुरुषाणाम् अर्थ इति पुरुषार्थः।
मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है वह धर्म, अर्थ काम एवं मोक्ष के
अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। परंतु इन चारों पुरुषार्थों में भी धर्म
सर्वोपरि है, क्योंकि वही समाज को धारण (Maintain) करने में समर्थ है।
धर्म-विरहित अर्थ (विजयाभिलाष) ने ही सम्राट अशोक से कलिंग का भयावह
नरसंहार कराया। धर्म-विरहित काम ने ही वेदज्ञ, शक्तिसंपन्न रावण को अंततः
विनाश के गर्त में धकेल दिया। धर्म-विरहित मोक्ष की कामना ने ही
विश्वामित्र को चिरकाल तक अशांत बनाए रखा। यही कारण है कि प्रत्येक
पुरुषार्थ का धर्म-समर्थित होना अनिवार्य है। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में
कहते हैं—
धर्माविरुद्धो भूतानां कामोऽस्मि पुरुषर्षम्
समय-समय पर ऋषि-मुनियों, शास्त्रकारों एवं कवियों ने धर्म को परिभाषित
किया। सामान्यतः जो (आत्मास्तित्व हेतु) धारण किया जाए, वही धर्म
है—ध्रियते इति धर्मः। महर्षि पतंजलि ने धर्म को इहामुत्रसाधक
तत्त्व निरूपित करते हुए कहा—यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस सिद्धिः स
धर्मः।
‘स्मृतिवाङ्मय’ में धर्म को व्यवहारिक स्तर पर
परिभाषित करते
हुए कहा गया—
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिमनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।
वस्तुतः धर्म को इसी व्यवहारिक पक्ष की लोक प्रतिष्ठा है, क्योंकि धैर्य,
क्षमाशीलता, कामनाओं पर नियंत्रण, अपरिग्रह, मनवाणी तथा कर्म की शुचिता,
इंद्रिय निग्रह, बुद्धि-विद्या (विवेक), सत्यपालन एवं क्रोध परिहार से ही
‘अभ्युदय’ की सिद्धि होती है। इन सद्गुणों
का
मनुष्य को प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक लाभ भी प्राप्त होता है।
धर्म-पालन से पारलौकिक श्रेयस अर्थात् मोक्ष की सिद्धि होना शब्द
प्रमाणाश्रित सत्य है। इसका कई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। फलतः उस संदर्भ
में लोगों का संदिग्ध-बुद्धि होना स्वाभाविक है। धर्मपालन से मोक्ष लाभ
होना विशुद्ध श्रद्धा एवं आस्था का विषय है। इसे तर्क से सिद्ध कर पाना
कठिन है—नैषा तर्केण मतिरापनीया।
भारतीय संस्कृति में धर्म को वृषभ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह धर्म की प्रतीकात्मक व्याख्या है। इस धर्मवृषभ के चार पाद हैं—सत्य, तप, यज्ञ और दान। पुराणों में इस संदर्भ की अनेकशः व्याख्या की गई है और बताया गया है कि कृतयुग में धर्म चतुष्पाद प्रतिष्ठत होता है। परंतु त्रेता, द्वापर एवं कलि में वह क्रमशः (तप, यज्ञ, दान) द्विपाद (यज्ञ एवं दान) तथा एकपाद (दान) रूप में ही स्थिर रहता है।
परंतु सत्यानुपालन, तत्पश्चर्या, यज्ञानुष्ठान तथा दान सबके वश का नहीं है। इसीलिए धर्माचरण को जनताजनार्दन की पहुँच तक लाने के लिए क्रांतिदर्शी आचार्यों में नाना प्रकार के व्रतानुष्ठानों, पुरश्चरणों, उपवासों एवं प्रायश्चित्तादि कर्मों की व्यवस्था की, जिसका विस्तृत वर्णन ‘निर्णयसिंधु’, ‘व्यवहारमय्रव’, ‘चतुर्वर्गचिन्तामणि’, ‘वीरमित्रोदय’ तथा ‘कृत्य कल्पतरु’ आदि ग्रंथों में उपलब्ध होता है।
व्रत शब्द वृ (धातु) में अतच् प्रत्यय जोड़कर निष्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य है किसी कार्य को करने का सुदृढ़ संकल्प अथवा प्रतिज्ञा। इसी प्रकार उपवास का तात्पर्य है शरीर शुद्ध के लिए अन्न न ग्रहण करना। उपवास के भी विविध रूप संभव हैं, जैसे-निर्जल उपवास अर्थात् जल तक न ग्रहण करना। पूर्ण उपवास अर्थात् सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक अन्न न ग्रहण करना। फलाहार अर्थात् उपवास की अवधि में मात्र फल ग्रहण करना। एकाहार अर्थात् पूरे दिन में कुछ न ग्रहण करके रात्रि-वेला में अन्न ग्रहण करना।
उपवास से जहाँ शरीर की शुद्धि होती है वहीं व्रतानुष्ठान से देवाराधना संभव होती है। व्रतों का यही व्यावहारिक पक्ष समाज में स्नेह, सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता तथा बंधुत्व आदि की सृष्टि भी करता है। क्योंकि अधिकांश व्रत पूर्णतः सामाजिक होते हैं। रामनवमी, कृष्णजन्माष्टमी, नवरात्र तथा शिवरात्रि के आते ही समूचा राष्ट्र मानो एक सामूहिक अह्लाद (Composit delight) में डूब जाता है। नागपंचमी, हरतालिका, करक चतुर्थी (करवा चौथ) लोलाक षष्टी एवं वटसावित्री आदि व्रतों में राष्ट्र का संपूर्ण नारी समाज एकरस हो उठता है।
समान्य आत्मपरितोष से लेकर अचिंत्य, असाध्य, दुष्प्राप्य लक्ष्य की प्राप्ति तक संभव है तो व्रत मात्र से। पुराणों में ऐसे विलक्षण व्रतों के अनेक दृष्टांत उपलब्ध हैं।’ श्रीमद्भागवत् पुराण’ (स्कंध 8, अध्याय 16) में देवमाता अदिति द्वारा संपादित केशवतोषण व्रत का अत्यंत हृदयग्राही वर्णन मिलता है। इसी कठिन व्रत के फलस्वरूप अदिति को वामन जैसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने देवराज इंद्र को उनका दानवापहृत साम्राज्य पुनः प्राप्त कराया। यह व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपत् तिथि से प्रारंभ कर बारह दिन तक किया जाता था। सिनीवाली (अमावस्या) की रात्रि में क्रोडविदारित मृत्तिका का शरीर पर लेप कर पृथ्वी की वंदना करते हुए स्नान करना चाहिए—
भारतीय संस्कृति में धर्म को वृषभ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह धर्म की प्रतीकात्मक व्याख्या है। इस धर्मवृषभ के चार पाद हैं—सत्य, तप, यज्ञ और दान। पुराणों में इस संदर्भ की अनेकशः व्याख्या की गई है और बताया गया है कि कृतयुग में धर्म चतुष्पाद प्रतिष्ठत होता है। परंतु त्रेता, द्वापर एवं कलि में वह क्रमशः (तप, यज्ञ, दान) द्विपाद (यज्ञ एवं दान) तथा एकपाद (दान) रूप में ही स्थिर रहता है।
परंतु सत्यानुपालन, तत्पश्चर्या, यज्ञानुष्ठान तथा दान सबके वश का नहीं है। इसीलिए धर्माचरण को जनताजनार्दन की पहुँच तक लाने के लिए क्रांतिदर्शी आचार्यों में नाना प्रकार के व्रतानुष्ठानों, पुरश्चरणों, उपवासों एवं प्रायश्चित्तादि कर्मों की व्यवस्था की, जिसका विस्तृत वर्णन ‘निर्णयसिंधु’, ‘व्यवहारमय्रव’, ‘चतुर्वर्गचिन्तामणि’, ‘वीरमित्रोदय’ तथा ‘कृत्य कल्पतरु’ आदि ग्रंथों में उपलब्ध होता है।
व्रत शब्द वृ (धातु) में अतच् प्रत्यय जोड़कर निष्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य है किसी कार्य को करने का सुदृढ़ संकल्प अथवा प्रतिज्ञा। इसी प्रकार उपवास का तात्पर्य है शरीर शुद्ध के लिए अन्न न ग्रहण करना। उपवास के भी विविध रूप संभव हैं, जैसे-निर्जल उपवास अर्थात् जल तक न ग्रहण करना। पूर्ण उपवास अर्थात् सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक अन्न न ग्रहण करना। फलाहार अर्थात् उपवास की अवधि में मात्र फल ग्रहण करना। एकाहार अर्थात् पूरे दिन में कुछ न ग्रहण करके रात्रि-वेला में अन्न ग्रहण करना।
उपवास से जहाँ शरीर की शुद्धि होती है वहीं व्रतानुष्ठान से देवाराधना संभव होती है। व्रतों का यही व्यावहारिक पक्ष समाज में स्नेह, सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता तथा बंधुत्व आदि की सृष्टि भी करता है। क्योंकि अधिकांश व्रत पूर्णतः सामाजिक होते हैं। रामनवमी, कृष्णजन्माष्टमी, नवरात्र तथा शिवरात्रि के आते ही समूचा राष्ट्र मानो एक सामूहिक अह्लाद (Composit delight) में डूब जाता है। नागपंचमी, हरतालिका, करक चतुर्थी (करवा चौथ) लोलाक षष्टी एवं वटसावित्री आदि व्रतों में राष्ट्र का संपूर्ण नारी समाज एकरस हो उठता है।
समान्य आत्मपरितोष से लेकर अचिंत्य, असाध्य, दुष्प्राप्य लक्ष्य की प्राप्ति तक संभव है तो व्रत मात्र से। पुराणों में ऐसे विलक्षण व्रतों के अनेक दृष्टांत उपलब्ध हैं।’ श्रीमद्भागवत् पुराण’ (स्कंध 8, अध्याय 16) में देवमाता अदिति द्वारा संपादित केशवतोषण व्रत का अत्यंत हृदयग्राही वर्णन मिलता है। इसी कठिन व्रत के फलस्वरूप अदिति को वामन जैसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने देवराज इंद्र को उनका दानवापहृत साम्राज्य पुनः प्राप्त कराया। यह व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपत् तिथि से प्रारंभ कर बारह दिन तक किया जाता था। सिनीवाली (अमावस्या) की रात्रि में क्रोडविदारित मृत्तिका का शरीर पर लेप कर पृथ्वी की वंदना करते हुए स्नान करना चाहिए—
त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता।
उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशाय।।
उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशाय।।
इस कठोर व्रत में अनुष्ठान का सांगोपांग पालन करने के साथ-ही-साथ जिस तथ्य
को सविशेष रेखांकित किया गया है, वह है किसी भी व्रत की अनिवार्यतः पालन
करने योग्य भूमिका। वस्तुतः वही भूमिका व्रतानुकूल मानसिकता की सृष्टि
करती है—
प्रतिपद्दिनमारम्य यावच्युक्लत्रयोदशी।
ब्रह्मचर्यमहाः स्वप्नं स्नानं त्रिषवणं चरेत्।।
वर्जयेदसदात्नापं भोगानुच्चावचांस्तथा।
अहिंसतः सर्वभूतानां वासुदेवपरायणः।।
मुक्तवत्सु च सर्वषु दीनान्धकृपणेषु च।
विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान् भुञ्जीत सह बन्धभिः।।
एतत्प्रयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परम्।
पितामहेनामिहितं मया ते समुदाहृतम।।
अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतम्।
तपः सारमिदं भद्रे ! दानं चेश्वरतर्पणम्।।
ब्रह्मचर्यमहाः स्वप्नं स्नानं त्रिषवणं चरेत्।।
वर्जयेदसदात्नापं भोगानुच्चावचांस्तथा।
अहिंसतः सर्वभूतानां वासुदेवपरायणः।।
मुक्तवत्सु च सर्वषु दीनान्धकृपणेषु च।
विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान् भुञ्जीत सह बन्धभिः।।
एतत्प्रयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परम्।
पितामहेनामिहितं मया ते समुदाहृतम।।
अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतम्।
तपः सारमिदं भद्रे ! दानं चेश्वरतर्पणम्।।
श्रीमद्भागवतकार केशवतोषण नामक इस पयोव्रतानुष्ठान को सर्वभूत, सर्वव्रत
तथा तपःसार पर्यायों से मंडित करते हैं, जिसका अर्थ मात्र यह है कि
केशवतोषण व्रत में समस्त व्रत अंतर्भूत हैं, समस्त यज्ञ अंतर्भूत हैं और
यह व्रत तपश्चर्या का सारभूत है।
व्रत का मूल उद्देश्य ही तप का संचय और भारतीय संस्कृति में तपस से परतर और कोई पदार्थ नहीं। ‘मनुस्मृति’ में तो तपश्शक्ति को ही सृष्टि का उपादान कारण मान लिया गया है। कठिन-से-कठिन कार्य की सिद्धि तपस से ही संभव है। पौराणिक वाङ्मय देवों, दानवों, गंधर्वों के विलक्षण तपोवृत्तांतों से ओत-प्रोत है।
विश्वामित्र द्वारा अपर स्वर्ग की सृष्टि, सशरीर त्रिशंकु का स्वर्गारोहण, वसिष्ठ द्वारा मात्र ब्रह्मदंड से विश्वामित्र की चतुरंगिणी सेना की पराजय, अगस्त्य द्वारा वातापि सहित सागर का पान—सबकुछ तप से ही सम्भव हुआ। स्मृतिकार मनु तो स्पष्टतः कहते हैं—
व्रत का मूल उद्देश्य ही तप का संचय और भारतीय संस्कृति में तपस से परतर और कोई पदार्थ नहीं। ‘मनुस्मृति’ में तो तपश्शक्ति को ही सृष्टि का उपादान कारण मान लिया गया है। कठिन-से-कठिन कार्य की सिद्धि तपस से ही संभव है। पौराणिक वाङ्मय देवों, दानवों, गंधर्वों के विलक्षण तपोवृत्तांतों से ओत-प्रोत है।
विश्वामित्र द्वारा अपर स्वर्ग की सृष्टि, सशरीर त्रिशंकु का स्वर्गारोहण, वसिष्ठ द्वारा मात्र ब्रह्मदंड से विश्वामित्र की चतुरंगिणी सेना की पराजय, अगस्त्य द्वारा वातापि सहित सागर का पान—सबकुछ तप से ही सम्भव हुआ। स्मृतिकार मनु तो स्पष्टतः कहते हैं—
तपोमूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखम्।
तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिमिः।।
यद्दुस्तरं यद्दुरापंयद्दुर्ग यच्चदुस्करम्।
सर्व तत्तापसा साध्यं तपो हि दुरतिक्षमम्।।
तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिमिः।।
यद्दुस्तरं यद्दुरापंयद्दुर्ग यच्चदुस्करम्।
सर्व तत्तापसा साध्यं तपो हि दुरतिक्षमम्।।
यही तप का प्रयोजनभूत है। कण्व-शिष्यों को आया हुआ सुनते ही वर्णाश्रम
धर्म-रक्षक दुष्यंत को पहली शंका यही होती है कि—किं तावद्
व्रतिनामुपोढतपसां विघ्नैस्तपो दृषितम्—अर्थात् कहीं ऐसा तो
नहीं है
कि तपस्संचय करनेवाले व्रती तापसों की तपस्या किन्हीं विघ्नों से खंडित
हुई (जिसकी शिकायत लेकर कण्व-शिष्य मेरे पास आए हैं), यहाँ कविकुलगुरु
कालिदास भी व्रतियों को उपोढ़ तपस मान रहे हैं। इस प्रकार व्रतोपवास का
मूल लक्ष्य है तपस अथवा आत्मशक्ति, आत्मऊर्जा की प्राप्ति। बिना
शक्ति-संचय के जीवन में कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है।
भारतीय व्रतानुष्ठान की यह उदात्त परंपरा निमागम से कंदलित एवं पल्लवित होकर पुराणवाङ्मय में न्यग्रोध विस्तृत हो गई। व्रतो तो व्रत है, चाहे वह एक सामान्य विद्यार्थी का स्वाध्यायव्रत हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अथवा देवी अदिति का दुष्कर पयोव्रत हो महामहिम शाली पुत्र (वामन) की प्रापित के लिए। सच तो यह है कि व्रतानुष्ठान कर्मयोग-पक्षधर भारतीय समाज की आधारशिला है। प्राध्यापक, कृषक, व्यापारी, व्यवसायी, साहित्यकार, कलाकार, राजनेता-सबके सब प्रकारांत से अपने-अपने व्रतानुष्ठान में लगे हैं।
भारतीय व्रतानुष्ठान की यह उदात्त परंपरा निमागम से कंदलित एवं पल्लवित होकर पुराणवाङ्मय में न्यग्रोध विस्तृत हो गई। व्रतो तो व्रत है, चाहे वह एक सामान्य विद्यार्थी का स्वाध्यायव्रत हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अथवा देवी अदिति का दुष्कर पयोव्रत हो महामहिम शाली पुत्र (वामन) की प्रापित के लिए। सच तो यह है कि व्रतानुष्ठान कर्मयोग-पक्षधर भारतीय समाज की आधारशिला है। प्राध्यापक, कृषक, व्यापारी, व्यवसायी, साहित्यकार, कलाकार, राजनेता-सबके सब प्रकारांत से अपने-अपने व्रतानुष्ठान में लगे हैं।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i