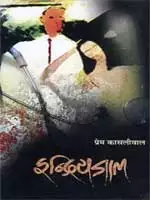|
सामाजिक >> इन्द्रियजाल इन्द्रियजालप्रेम कासलीवाल
|
17 पाठक हैं |
|||||||
एक श्रेष्ठ उपन्यास
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
बाम्बे-आगरा राजमार्ग के आधा किलोमीटर टुकड़े के किनारे बने कुछ पक्के
मकानों और कुछ झोपड़ों के जमावड़े को गाँव कहना चाहें तो कह सकते हैं, न
चाहें तो, मर्जी। वैसे गाँव जैसा सब कुछ तो नहीं है, पर कुछ तो था
ही—कम से कम गाँव वालों की नजरों में तो बहुत कुछ था। सबसे बड़ी
बात और सौ बातों की एक बात—ए.बी. रोड पर बसा था। अधिकांश गाँव
वालों का इंग्लिश भाषा से परिचय ‘ए’ और ‘बी’ तक ही जाता था।
एक-दो किराने वालों की दुकान, एक कपड़े की दुकान और बाकी घर। धोबी, नाई से लेकर पान-बीड़ी वालों और सायकल सुधारने वालों की दुकान जैसा कुछ नहीं। घर में जाओ—पान बीड़ी ले आओ या सायकल के ब्रेक कसा लो। गाँव में ‘ब्रेक’ टाइट नहीं होते, कसे जाते थे। रौनक थी तो बस ए.बी. रोड की वजह से। दिनभर में दो-तीन बसें, पाँच-दस ट्रक और अधिकतर बैलगाड़ियाँ आवाज करती गुजरतीं। सबसे बड़ा ‘सरकारी’ घर था—लम्बे बरामदे और एक हॉल जिसमें डेढ़ कमरे भी बने थे। ‘घर’ यूँ कहने में आया कि उसमें कई घर थे जैसे दवाघर, शिक्षाघर और आधे कमरे में छोटा-सा मन्दिर याने देवघर। इस बड़े घर में आपसी सामंजस्य की बेमिसाल इमारत थी। दवाघर का कम्पाउंडर याने गाँव का ‘डाकसाब’ रंग-बिरंगे, ‘मिक्चर’ बनाता, बाँटता, गोलियों को खरल में पीसकर दुगनी पुड़िया तो बनाता ही, आवश्यकता पड़ जाने पर एक हेड मास्टर और एक मास्टर वाले शिक्षाघर में जाकर जब तब छड़ी भी पकड़ लेता। जिन लौंडे-लपाड़ों को स्कूल में आना ही पड़ता, उनके हाथों से ‘माँ सरस्वती’ फिसल जाती। मास्टर सा’ब के पास भी न जाने कहाँ का ‘आर्युवेद-रत्न’ पत्थर-सा दबा था। ‘डाकसाब’ नहीं होते तो ‘रतन’ जमीन फाड़ कर ऊपर आ जाता था। उसका रंग भी ‘मिक्चर’ से मिलता था। हेडमास्टर साहब धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, इसलिए उनका ज्यादातर वक्त देवघर में ही गुजरता, शेष पढ़ाने में और डाकघर का काम देखने में। घूमते-फिरते पहली से आठवीं तक की क्लास भी लेते और पोस्टकार्ड, टिकिट और लिफाफे भी बेचते। डाकघर का शेष काम लड़के शौक से करते। बाहर लगे लेटर बॉक्स से चिट्ठियाँ निकालना, मोहर ठोकना, थैले में भर सुतली से मुँह बन्द कर गरम लाख से सील करना आदि। चिट्ठियों पर पोस्ट ऑफिस का ठप्पा लगाने के लिए बच्चे आपस में झगड़ते और हेड-मास्टर साब को एक-दो गालों पर या पीठ पर ‘ठप्पा’ ठोकना पड़ता था। उसमें तारीख होती ही नहीं, किसी को याद रहती नहीं। स्कूल में ज्यादातर बच्चे वे होते जिनके घर में काम नहीं होता या जिनके पिताजी को भी करने को कुछ खास काम नहीं होता। किसी घर की स्थिति किसी दिन उलटी होती तो उस घर का चिराग घर में ही रोशनी देने के लिए रोक लिया जाता। उपस्थिति के मामले में हेडमास्टर साब उदार थे। गाँव के दोनों छोरों पर रहनेवाले छोकरों को चिट्ठियाँ थमा देते। डाक बँट जाती। फिर क्यों किसी के नाम के आगे अँगरेजी का ‘ए’ लिखना।
गाँव में अखबार भी आता था। दो या तीन कॉपी। शाम तक कभी भी। यह बस के ड्राइवर या कंडेक्टर पर निर्भर करता था कि बस रोके या न रोके, अखबार जाते या वापस पलटते वक्त फेंके। कहां फेंके, यह इस बात पर निर्भर होता कि सवारी को, यदि होती तो किस घर के सामने उतरना होता और नहीं होती तो बस की रफ्तार पर निर्भर करता। बहरहाल, अखबार का बंडल दिन में कभी भी ए.बी. रोड के एक किलोमीटर के टुकड़े के किनारे पर पड़ा मिल जाता। जिसे मिलता बिना खोले रतनदादा, बड़े सोनीजी और मन्त्रीजी के घर पहुँच जाता। तीनों घरों में ग्राम पंचायत का ऑफिस था। बोर्ड सरपंचजी ने अपने घर के ओसारे में लगा रखा था। खबरें सुनने में ज्यादा आनन्द आता—मजबूरी थी ही। बिना नागा, शाम को मन्त्रीजी के घर पहुँच जाते। मन्त्रीजी महाभारत की कथा सुनाते। सरपंचजी ‘रामायण पाठ’ की तरह लगन और भक्ति भाव से सुनते। मुश्किल हाट के दिन होती। खबरें फट कर नून, मिर्ची, मसाले या गुड़ का जायका लेतीं। पता भी नहीं चलता क्योंकि पंचायत जुटती ही नहीं। अपनी रोटी-दाल के जुगाड़ में भिड़ी होती।
खैर, बात ‘इसकूल’ की थी। वह साल-दर-साल ‘इसकूल’ ही बना रहा काकाजी के लिए ! गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल का घण्टा बजा तो काकाजी ने कहा, ‘‘जा—‘इसकूल’ जा...बहुत मटरगश्ती हो गयी।’’ वह गया और लौटकर आ गया। काकाजी ने पूछा, ‘उसने बता दिया। काकाजी हेडमास्टर के पास गये तब उन्हें पता लगा कि गाँव के ‘इसकूल’ की एक किस्म ‘मिडिल इसकूल’ होती है और उन्हें आगे पढ़ाना है तो ‘हाई-स्कूल’ भेजना होगा याने गाँव बदर...। काकाजी ने सुना और चले आये। हाई-स्कूल ‘हाई’ तो था ही, ‘हाय’ स्कूल भी। ‘‘आठ किलास भन लिया...भोत है।’’
‘‘जा जल्दी से जीम ले। हाट का दिन है।’’ और दुकान जमाने में व्यस्त हो गये। छः बाय चार की दुकान में दो-चार थान चौल, लट्ठा, साटन और दीगर सामान के अलावा गज और कैची थे। ‘हाथ’ नहीं था। कुहनी से मध्यमा की दूरी हाथ भर की थी। काम चल जाता।
वह जीमने अन्दर चला गया। काकाजी कपड़े के थानों को इस तरह रखने लगे कि दुकान भारी-भारी लगे और ग्राहकों को बैठने की जगह भी रहे। हालाँकि दुकान में माल ज्यादा तो नहीं होता परन्तु छः बाय चार की दुकान में काकाजी को मशक्कत करनी होती—खास कर हाट के दिन। ग्राहक संख्या में तो कम होते परन्तु बैठने की जगह होने से सौदा करने में जल्दी नहीं करते। धोती के लिए लट्ठा लेना होता तब भी चौल का थान खुलवाते और बीड़ी फूँकते बैठे रहते।
स्कूल लगा होता तो भी उसे आधा दिन का नागा करना पड़ता, ‘‘यही काम आएगा।’’ काकाजी कहते। गज या हाथ से कपड़ा नापना, कैंची लगाकर चट्ट से फाड़ना, घरी करना, थान को लपेटना और पैसे लेना-देना भी। इस तरह पढ़ता भी और पैतृक व्यवसाय के गुण भी, गुर भी सीखता रहता था।
रसोईघर घर के ठीक पिछले हिस्से में था। बाई अधिकांश रसोईघर में होती। गाय को सुबह चरने छोड़ देती और रसोई में जुट जाती। शाम को गाय की घंटी सुनती, चौका समेटती और तब रसोईघर से बाहर निकल पाती। स्कूल की घंटी उसे सुनाई नहीं पड़ती। दो दिन तक तो बाई का ध्यान ही नहीं गया कि वह दिनभर या तो दुकान पर कपड़े फाड़ता है, शाम को सिल्लक मिलाता है और या फिर मटरगश्ती करने को निकल जाता है। इस बीच काकाजी पास के कस्बे से दो बोरी नाज की और पुरानी तराजू बाट भी ले आये थे। वह कपड़े नापता तो काकाजी नाज तोलते—हाथ बढ़े तो आमदनी भी बढ़नी चाहिए कि नहीं। फिर उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया। हाट-बाजार के दिन दुकान तो देखता ही था और दूसरे दिनों में गाँवभर में भटकने, मटरगश्ती करने और पीछे नदी के आसपास उगे झाड़-झंखाड़ों के बीच से बेर, जामुन, इमलियाँ बटोरने की आजादी तो थी ही। पहले जैसी। बस, चिट्ठियों पर मोहर ठोंकने में मस्त हो गया था....
दुकान और कोठारे के बीच एक भारी दरवाजा था जो हमेशा खुला रहता था। उसके एक पलड़े पर साँकल लटकी थी, दरवाजा बन्द करने के लिए नहीं, खटखटाने के लिए। बाई के लिए लगवा दी थी। पहले दरवाजे हिलते भी तो तीखी ‘चरर’ की आवाज होती और काकाजी को ‘खबर’ मिल जाती। उठते और रसोई घर की ओर चले जाते ‘खाना लग गया’। तब फर्श कच्चा था। काकाजी ने लाल पत्थर का मोटा फर्श लगवा लिया था। न अनगढ़ मेशन ने ध्यान दिया, न काकाजी ने मोटी फर्शियाँ इतनी ऊँची लग गयीं कि दरवाजे के बन्द होने की तो क्या हिलने की सँभावना भी खत्म हो गयी। तब, काकाजी ने मोटी, लोहे की साँकल लगवा दी।
तीसरे दिन बाई का ध्यान गया...एक बार नहीं, दो बार नहीं...तीन बार साँकल खड़खड़ाई, जोर-जोर से। बाई साँकल पकड़े दरवाजे की ओट में खड़ी रही।
खटखटाकर अन्दर रसोई में नहीं गयी।
काकाजी दुकान में नहीं थे।
‘क्यों रे...तू इसकूल नहीं गया ?’’ बाई ने गुस्से में पूछा और उसे ओसारे में आने का इशारा किया।
‘‘मास्टर ने मना कर दिया।’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘क्या मालूम।’’ उसने लापरवाही से कहा, ‘‘काकाजी को मालूम है।’’
बाई ओसारे में खड़ी उबली और रसोईघर तक उफनती चली गयी—‘‘भणेगो नहीं...कपड़ा फाड़ेगो....’’
दूसरे दिन काकाजी ने ओसारे में दरी बिछायी और उसके एक सिरे पर उसके सोने, बिछाने, ओढ़ने और पहनने के कपड़े रखे और दरी में लपेटकर लम्बी सुतली से कसकर बाँध दिया और बिस्तरबन्द को हाथ में उठाये उसे फाटे तक ले गये और धार जानेवाली बस में बैठा दिया, ‘‘सीधे घर जाना...किसी से भी वकील साब का घर पूछ लेना...ताँगा मत करना...।’’ उसकी हथेली में पाँच-पाँच के दो नोट और कुछ सिक्के रखे थे जो बस के किराये और स्कूल फीस के लिए थे। चाचाजी का घर था ही रहने-खाने के लिए। बिस्तरबन्द में पाजामा, कमीज की जोड़ी थी ही। एक नयी। कल शाम को ताबड़तोड़ बनवायी थी। दादा छुटपन से ही चाचाजी के यहाँ पढ़ रहे थे।
गाँव की दुनिया से निकल कुछ बड़ी दुनिया में घुसते ही जिन दो चीजों पर पहली बार नजर पड़ी वे थीं—‘ताँगे’ और पक्का ‘मोहन टॉकीज’। गाँव में ताँगे न ण्थे। वहीं थीं किराये की सायकल या साल दो साल में आने वाली नौटंकी। बहरहाल, वह एकान्तर घर से पूछता-पूछता शनि मन्दिर की गली में पहुँच गया। दादा बाहर ही खेल रहे थे। राहत की साँस ली।
उसे इतना ही मालूम था कि अब स्कूल नहीं, हाईस्कूल जाना है, आगे पढ़ने के लिए। किताबों से पहले दादा ने उसके नंगे पैरों को हवाई-चप्पलों में डाला और नाई के पास ले गये। नाई की दुकान देखकर चौंका। आइने के सामने कुर्सी पर बैठा था और कुर्सी के हत्थे कसकर पकड़ रखे थे। नाई बाल काटता जाता और कुर्सी के इर्द गिर्द घूमता जाता। उसे नहीं घूमना होता। बार-बार गाँव के रामप्रसाद काका का रौबीला चेहरा याद आता रहा : ‘‘सीधे बैठ..इधर घूम...उधर घूम...उधर झुक...।’’ बालों की लम्बाई रामप्रसाद काका की मर्जी और उसके बिना हिले-डुले, चीखे-चिल्लाए बाल कटते देखने की शक्ति पर निर्भर करती।
स्कूल का प्रवेश-फार्म दादा ने भरा, इसलिए स्कूल जाने के बाद मालूम पड़ा कि गणित में अच्छे नम्बरों के बावजूद उसे बायलॉजी पढ़ना है। समझ नहीं आया कि आखिर पढ़ना क्या पढ़ेगा। बायलॉजी की एक किताब देख राहत महसूस की अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित की तीन-तीन किताबों में सर फोड़ने के बजाय एक ही किताब से माथापच्ची करनी होगी और उसमें भी निर्जीव आँकड़ों और रेखाओं का जाल नहीं होगा। फूल होंगे, पत्तियाँ होंगी या मेंढक-मच्छर। गाँव की नदी के किनारे उगी झाड़ियों के जंगल से दूर हो जाने का गम कुछ तो कम हुआ।
आँकड़ों की दुनिया से छुटकारा तो मिला परन्तु पूरी तरह नहीं। दशहरा-दीवाली और गर्मियों की छुट्टियों में जब भी घर आता—दुकान के बही चौपड़ों से उलझना पड़ता। कुढ़न होती। सोचता, गर्मियों की छुट्टियाँ क्यों होती हैं...और होती हैं तो इतनी लम्बी क्यों...। काकाजी के साथ शाम को लालटेन की रोशनी में सिल्लक गिनते हुए पता नहीं कब वह अपने सपने देखने ही नहीं...गिनने भी लगा...वह स्कूल से निकल कॉलेज की सीढ़ियाँ चढ़ने को आतुर होता...काकाजी उसके, ‘इसकूल’ के सहपाठियों की तारीफ के पुल बाँधने लगते जो स्कूल की सीढ़ियाँ उतरते ही अपने खानदानी व्यवसाय में पीढ़ी-दर-पीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे थे। आमदनी वही हो, पर ‘कमा’ रहे थे।
अब उसे कोफ्त होती। स्कूल के साथी कामकाज में जुटे थे और मन मसोस कर ही उसे दुकान पर बैठना पड़ता, लट्ठा नापना पड़ता, साटन फाड़ना पड़ती। हिसाब लगा कर पैसे लेने-देने पड़ते। आँकड़े चुभते। बही चौपड़े लिखने में गड़बड़ी होती ही होती और काकाजी की डाँट सुननी ही पड़ती, ‘पता नहीं ‘हायस्कूल’ में क्या पढ़ाते हैं...इससे तो ‘इसकूल’ अच्छा था...बिस्तर बाँध यहीं आजा...भैया...’
‘इसकूल अच्छा था’ के आगे पापा कहते तो नहीं कि फीस भी नहीं लगती थी परन्तु लगता आर्थिक थकान आवाज में उतर आयी है।
वह कभी सोचता भी...हाईस्कूल और बस। बहुत पढ़ लिया।
दादा धार छोड़ कर इन्दौर चले गये। कॉलेज से भी बड़े कॉलेज पढ़ने यानी पी.जी. करने। वहाँ चचेरी बहन की ससुराल थी—यानी रहना फ्री, खाना फ्री। कपड़े तो यूँ भी लगते ही हैं—पढ़ो या न पढ़ो। दादा इन्दौर जा सकते हैं तो वह भी...
सपने बढ़ने लगे। गिनती करना मुश्किल ही नहीं, पीड़ादायक था। काकाजी की थकी आवाज कानों में भरी रहती और आँकड़ों में तो वह गलती करने लगा ही था।
ऐसे ही दुकान पर बैठे उसने काकाजी को बाई से कहते सुना, ‘‘बही-चौपड़े लिखना नहीं सीखेगा तो दुकान कैसे चलाएगा...बाद में।’’ काकाजी जानबूझकर नहीं कहते, ‘‘मेरे बाद में।’ बाई साड़ी का पल्लू आँखों पर रगड़ने लगती थी—
‘‘छुट्टी में आया है...सीखने में क्या हर्ज है...काम आएगा कभी न कभी।’’
बाई को भी लगता—सीखने की ही बात है...तो सीख लेने दे। चुपचाप रसोई में चली जाती।
घर में दो बुआएँ और दूर के मामा का लड़का भी रहता था। बही-खाते मिलाते हुए उसकी आँखें फटी की फटी रह गयीं, ‘इस छः बाय चार की दुकान की उससे भी कहीं छोटी, आमदनी में काकाजी पाँच लोगों का खर्च और उनकी पढ़ाई का खर्च कैसे चलाते होंगे...’
उसे लगा, उम्र और हिसाब दोनों में वह कच्चा है और पढ़-पढ़ कर आँखें भी कमजोर हो गयी हैं। बही-खातों में तो आँकड़े लिखे थे परन्तु एक बहुत पीड़ा-जनक राज़ बाई और काकाजी आँखों में छुपा था।
उस दिन बस का ड्राइवर अखबार के बण्डल के साथ काकाजी के नाम दादा की चिट्ठी भी फेंक गया। चिट्ठी कागज का खुला पुर्जा था। बड़े सोनीजी ने देखा तो अपने घर से ही जोरदार आवाज में चिट्ठी काकाजी को सुना दी, ‘‘मनु का मेडिकल में एडमीशन हो गया है...फार्म और फीस जल्दी भरना है। मनु को जल्दी से इन्दौर रवाना करना...। सब को ढोक !’’
उत्तेजना में वह बड़े सोनीजी के घर की तरफ भागा। चिट्ठी को जेब में रखा और अखबार के पन्ने टटोलने लगा। चयनित छात्रों में उसका नाम था। उसने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का फोटो भी नहीं देखा और देखते ही देखते वह गाँवभर का ‘डॉक्टर’ बन गया।
उसने सपने तो बहुत देखे थे...या देखे कम, गिने ज्यादा थे। याद नहीं आया कि यही सपना उसने देखा था। अब लग रहा था—यही उसका सपना था जो उसने कभी देखा ही नहीं था।
कुछ देर बाद काकाजी अखबार थामे भारी पैरों को घसीटते धीरे-धीरे चलते घर पहुँचे। माथे पर शिकनों का हुजूम लगा था।
एकाएक मुखर हो गयी बाई पड़ोसिनों से बधाई लेने में इतनी व्यस्त थी कि कब काकाजी रसोई में आकर, बिना चटाई बिछाए बैठ गये, पता नहीं चला। उस दिन काकाजी को रसोईघर की साँकल बजानी पड़ी। बाई ने थाली लगायी। काकाजी ने मुँह जूठा किया और उठ गए। कभी खाने की थाली में जूठन का एक दाना भी नहीं छोड़नेवाले काकाजी भरी थाली छोड़ दुकान में गये और खाली बही-खाते टटोलने लगे। अँतड़ियाँ कम, आँखें ज्यादा जल रही थीं।
कील से मन्दिर के दरवाजे की चाबी उतारी और चले गये।
अगले दो दिन सन्नाटे से भरे थे। कोई कुछ नहीं बोलता। बस दुकान में लट्ठे-साटन के फटने और रसोईघर में बर्तनों की उठापटक की आवाज होती। धीरे-धीरे फटने की आवाज रसोईघर तक पहुँचने लगी और उससे भी दुगनी रफ्तार से बर्तनों के पटकने की आवाज दुकान में भी सुनाई पड़ने लगी। काकाजी दमा के मरीज की तरह हवा पीते। गले में सूखी हवा भी फँस जाती और देर तक खाँसते रहते। आँखों में पानी आ जाता।
उन दिनों काकाजी ने उम्र के कई साल जी लिये। चेहरा झुर्रियों से अटा था, आँखें और धँस गयी थीं और गालों की हड्डियाँ चेहरे के रेगिस्तान में ढूहों सी उभरी थीं। आँखें खुलतीं तो खुली रहतीं, बन्द होतीं तो पलकों के अन्दर पुतलियाँ कंचे की गोलियों की तरह लुढ़कती रहतीं।
सन्नाटा टूटता नहीं। बाई के साँकल खड़खड़ाने की अवधि बढ़ती गयी। काकाजी हड़बड़ाकर उठते और खड़े रहते। भारी पैरों को उठा भी नहीं पाते..आगे बढ़ाने की बात तो दूर रही। बाई ओसारे में खड़ी साँकल झकझोरती रहती।
उससे तो काकाजी ने न कुछ कहा, न पूछा। बाई की आँखें जरूर बोलती सी लगतीं, तू फिकर मत कर रे...।
तीसरे दिन वह दुकान पर बैठा था। तभी काकाजी आते दिखे। अभी तो मन्दिर गये थे...? उसने घड़ी देखी—आठ ही बजे थे। दस से पहले तो काकाजी मन्दिर से नहीं आते ? अनायास ही उसने बही खोल ली।
काकाजी ने झुककर देहरी छुई, हथेली को माथे से लगाया, ‘‘रहने दे...जा, जल्दी से नहा-धो ले...खाना खा ले...दस बजे बस आती है, इन्दौर की...जल्दी कर...बस जल्दी भी आ जाती है।’’
अन्दर गया। बाई बिना नहाये-धोये, मन्दिर गये, फुलके सेंक रही थी यानी ‘पाप’ कर रही थी। चूल्हे से उठतीं लपटों में ‘पाप’ जल रहा था और बाई का चेहरा दिपदिपा रहा था।
ओसारे में काकाजी ने फिर दरी बिछायी और उसके बीच ओढ़ने, बिछाने की चीजें रख बिस्तरबन्द बनाया और कसकर बाँधा—सुतली से। फिर डाकघर गये—थोड़ा-सा लाख लाने के लिए। मुहर लगाने के लिए—अँगूठा था ही !
पहली बार की तरह, दूसरी बार भी मनु का, बिस्तरबन्ध बँधा—कभी-कभी ही मुँह खोलनेवाली बाई के ‘कहने’ पर।
कब बस ने गुजरी की सीमा पार की और कब राष्ट्रीय राजमार्ग ‘ए.बी.’ रोड पर दौड़ती-हाँफती, हिचकोले खाती इन्दौर की शहर-सीमा में घुसी, पता ही नहीं चला। बस खचाखच सवारियों से भरी थी और मनु बीच-रास्ते में बिस्तरबन्द पर बैठा, जैसे-तैसे अपने को गिरने लुढ़कने से बचाते हुए। बाहर का कुछ नजर नहीं आ रहा था। सारे रास्ते बस के फर्श पर आड़े-तिरछे खड़े पैरों, जूतों और हवाई चप्पलों को देखता रहा। किसी का ध्यान मनु की ओर था ही नहीं—यहाँ तक कि खुद मनु का। मनु के पैर ही नहीं, वह खुद भी ‘हवाई-चप्पलों’ में सफर कर रहा था। बस स्टैण्ड पर पहुँच गयी और उसे पता ही नहीं चला कि कब वह बिस्तरबन्द पर अधलेटा मेडिकल कॉलेज के सामने से गुजर गया।
पहले दिन मनु कॉलेज जा नहीं पाया। कपड़े नहीं थे। कपड़े यानी प्रथम वर्ष, मेडिकल स्टूडेंट का गणवेश। बिस्तरबन्द में वे ही कपड़े काकाजी ने बाँध दिये थे जिन्हें पहनकर वह स्कूल भी गया था और एक साल कॉलेज भी। रंगीन धारीदार कमीज की जोड़ी और सफेद पापलीन के पायजामे। कमीज सफेद झक्क चाहिए थी—लेकिन रंगीन थी और ऊपर से धारीदार। पायजामे सफेद थे—चाहिए पैंट थे। जूते-मोजे तो रेडीमेड मिल गये परन्तु पैंट-शर्ट सिलने को टेलर को दिये थे। दुकान का साप्ताहिक अवकाश था। गया और आ गया। दादा ‘डरना नहीं’ कहकर बहुत पहले ही कॉलेज चले गये थे और वह अधखुले बिस्तरबन्द पर बैठा ‘क्या करे’ सोचता रहा। कमीज-पायजामे में तो कॉलेज जा नहीं सकता था। दादा का कहना था !
नहाकर भी क्या करेगा...सोच, बहुत देर तक नहाना स्थगित करता रहा। बिस्तरबन्द टटोलता रहा—टॉवेल था ही नहीं। ‘चन्दू’ (काकाजी को चन्दू ही कहकर बुलाते थे) के पास होगा ही...। एक टॉवेल से दो बदन क्यों नहीं पोंछे जा सकते, यही सोच काकाजी ने बिस्तरबन्द में नया टॉवेल नहीं रखा होगा—मनु ने सोचा।
कपड़े होते हुए भी, ड्रेस नहीं है। ड्रेस नहीं, इसलिए कॉलेज नहीं जा सकता—अजीब लग रहा था मनु को। यह भी कोई बात हुई ? कोई नंगा तो नहीं जाता ! या कमीज पायजामा पहनकर जाने से—कॉलेज ‘नंगा’ हो जाता ? स्कूल तो नहीं हुआ, और धार में एक साल कॉलेज में भी कमीज-पायजामे में ही गया—वह भी पैरों में हवाई-चप्पल पहने। न मनु हवाई-चप्पल पहन उड़ा, न स्कूल-कॉलेज की बिल्डिंग जमीन में धँसी। पता नहीं, कैसे ईंट-चूने से बनी थी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और कैसी थीं कॉलेज की दीवारें ! सफेद ? पता नहीं। बस में सीट पर बैठा होता तो शायद दीख जाती। कॉलेज के पहले दिन ही—तड़ी।
कल शाम को दादा दो सीनियर्स को मिलाने लाये थे।
‘‘तो यह है नया पंक्षी।’’ दोनों ने एक साथ चहकते हुए उसका अभिवादन का जवाब मनु की पीठ पर ‘धौल’ जमाते हुए दिया था।
मनु ने दादा की ओर देखा। ‘पंक्षी ? कौन ? मनु ने दोनों बाँहों की जगह टटोला—
‘‘देख क्या रहा है...पैर छू...सीनियर्स हैं।’’ दादा खुद सीनियर्स बन आदेश दे रहे थे।
मनु को सिर, गरदन, पीठ और हाथ झुकाने पड़े। न जान-पहचान, न आदर-सम्मान फिर भी...?
‘‘वेल, बी.सी. (दादा का नाम), पंक्षी की ट्रेनिंग शुरू कर दी...’’ एक सीनियर जिसके हाथ में मोटी-सी किताब थी, कु्र्सी पर बैठते हुए बोला।
एक-दो किराने वालों की दुकान, एक कपड़े की दुकान और बाकी घर। धोबी, नाई से लेकर पान-बीड़ी वालों और सायकल सुधारने वालों की दुकान जैसा कुछ नहीं। घर में जाओ—पान बीड़ी ले आओ या सायकल के ब्रेक कसा लो। गाँव में ‘ब्रेक’ टाइट नहीं होते, कसे जाते थे। रौनक थी तो बस ए.बी. रोड की वजह से। दिनभर में दो-तीन बसें, पाँच-दस ट्रक और अधिकतर बैलगाड़ियाँ आवाज करती गुजरतीं। सबसे बड़ा ‘सरकारी’ घर था—लम्बे बरामदे और एक हॉल जिसमें डेढ़ कमरे भी बने थे। ‘घर’ यूँ कहने में आया कि उसमें कई घर थे जैसे दवाघर, शिक्षाघर और आधे कमरे में छोटा-सा मन्दिर याने देवघर। इस बड़े घर में आपसी सामंजस्य की बेमिसाल इमारत थी। दवाघर का कम्पाउंडर याने गाँव का ‘डाकसाब’ रंग-बिरंगे, ‘मिक्चर’ बनाता, बाँटता, गोलियों को खरल में पीसकर दुगनी पुड़िया तो बनाता ही, आवश्यकता पड़ जाने पर एक हेड मास्टर और एक मास्टर वाले शिक्षाघर में जाकर जब तब छड़ी भी पकड़ लेता। जिन लौंडे-लपाड़ों को स्कूल में आना ही पड़ता, उनके हाथों से ‘माँ सरस्वती’ फिसल जाती। मास्टर सा’ब के पास भी न जाने कहाँ का ‘आर्युवेद-रत्न’ पत्थर-सा दबा था। ‘डाकसाब’ नहीं होते तो ‘रतन’ जमीन फाड़ कर ऊपर आ जाता था। उसका रंग भी ‘मिक्चर’ से मिलता था। हेडमास्टर साहब धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, इसलिए उनका ज्यादातर वक्त देवघर में ही गुजरता, शेष पढ़ाने में और डाकघर का काम देखने में। घूमते-फिरते पहली से आठवीं तक की क्लास भी लेते और पोस्टकार्ड, टिकिट और लिफाफे भी बेचते। डाकघर का शेष काम लड़के शौक से करते। बाहर लगे लेटर बॉक्स से चिट्ठियाँ निकालना, मोहर ठोकना, थैले में भर सुतली से मुँह बन्द कर गरम लाख से सील करना आदि। चिट्ठियों पर पोस्ट ऑफिस का ठप्पा लगाने के लिए बच्चे आपस में झगड़ते और हेड-मास्टर साब को एक-दो गालों पर या पीठ पर ‘ठप्पा’ ठोकना पड़ता था। उसमें तारीख होती ही नहीं, किसी को याद रहती नहीं। स्कूल में ज्यादातर बच्चे वे होते जिनके घर में काम नहीं होता या जिनके पिताजी को भी करने को कुछ खास काम नहीं होता। किसी घर की स्थिति किसी दिन उलटी होती तो उस घर का चिराग घर में ही रोशनी देने के लिए रोक लिया जाता। उपस्थिति के मामले में हेडमास्टर साब उदार थे। गाँव के दोनों छोरों पर रहनेवाले छोकरों को चिट्ठियाँ थमा देते। डाक बँट जाती। फिर क्यों किसी के नाम के आगे अँगरेजी का ‘ए’ लिखना।
गाँव में अखबार भी आता था। दो या तीन कॉपी। शाम तक कभी भी। यह बस के ड्राइवर या कंडेक्टर पर निर्भर करता था कि बस रोके या न रोके, अखबार जाते या वापस पलटते वक्त फेंके। कहां फेंके, यह इस बात पर निर्भर होता कि सवारी को, यदि होती तो किस घर के सामने उतरना होता और नहीं होती तो बस की रफ्तार पर निर्भर करता। बहरहाल, अखबार का बंडल दिन में कभी भी ए.बी. रोड के एक किलोमीटर के टुकड़े के किनारे पर पड़ा मिल जाता। जिसे मिलता बिना खोले रतनदादा, बड़े सोनीजी और मन्त्रीजी के घर पहुँच जाता। तीनों घरों में ग्राम पंचायत का ऑफिस था। बोर्ड सरपंचजी ने अपने घर के ओसारे में लगा रखा था। खबरें सुनने में ज्यादा आनन्द आता—मजबूरी थी ही। बिना नागा, शाम को मन्त्रीजी के घर पहुँच जाते। मन्त्रीजी महाभारत की कथा सुनाते। सरपंचजी ‘रामायण पाठ’ की तरह लगन और भक्ति भाव से सुनते। मुश्किल हाट के दिन होती। खबरें फट कर नून, मिर्ची, मसाले या गुड़ का जायका लेतीं। पता भी नहीं चलता क्योंकि पंचायत जुटती ही नहीं। अपनी रोटी-दाल के जुगाड़ में भिड़ी होती।
खैर, बात ‘इसकूल’ की थी। वह साल-दर-साल ‘इसकूल’ ही बना रहा काकाजी के लिए ! गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल का घण्टा बजा तो काकाजी ने कहा, ‘‘जा—‘इसकूल’ जा...बहुत मटरगश्ती हो गयी।’’ वह गया और लौटकर आ गया। काकाजी ने पूछा, ‘उसने बता दिया। काकाजी हेडमास्टर के पास गये तब उन्हें पता लगा कि गाँव के ‘इसकूल’ की एक किस्म ‘मिडिल इसकूल’ होती है और उन्हें आगे पढ़ाना है तो ‘हाई-स्कूल’ भेजना होगा याने गाँव बदर...। काकाजी ने सुना और चले आये। हाई-स्कूल ‘हाई’ तो था ही, ‘हाय’ स्कूल भी। ‘‘आठ किलास भन लिया...भोत है।’’
‘‘जा जल्दी से जीम ले। हाट का दिन है।’’ और दुकान जमाने में व्यस्त हो गये। छः बाय चार की दुकान में दो-चार थान चौल, लट्ठा, साटन और दीगर सामान के अलावा गज और कैची थे। ‘हाथ’ नहीं था। कुहनी से मध्यमा की दूरी हाथ भर की थी। काम चल जाता।
वह जीमने अन्दर चला गया। काकाजी कपड़े के थानों को इस तरह रखने लगे कि दुकान भारी-भारी लगे और ग्राहकों को बैठने की जगह भी रहे। हालाँकि दुकान में माल ज्यादा तो नहीं होता परन्तु छः बाय चार की दुकान में काकाजी को मशक्कत करनी होती—खास कर हाट के दिन। ग्राहक संख्या में तो कम होते परन्तु बैठने की जगह होने से सौदा करने में जल्दी नहीं करते। धोती के लिए लट्ठा लेना होता तब भी चौल का थान खुलवाते और बीड़ी फूँकते बैठे रहते।
स्कूल लगा होता तो भी उसे आधा दिन का नागा करना पड़ता, ‘‘यही काम आएगा।’’ काकाजी कहते। गज या हाथ से कपड़ा नापना, कैंची लगाकर चट्ट से फाड़ना, घरी करना, थान को लपेटना और पैसे लेना-देना भी। इस तरह पढ़ता भी और पैतृक व्यवसाय के गुण भी, गुर भी सीखता रहता था।
रसोईघर घर के ठीक पिछले हिस्से में था। बाई अधिकांश रसोईघर में होती। गाय को सुबह चरने छोड़ देती और रसोई में जुट जाती। शाम को गाय की घंटी सुनती, चौका समेटती और तब रसोईघर से बाहर निकल पाती। स्कूल की घंटी उसे सुनाई नहीं पड़ती। दो दिन तक तो बाई का ध्यान ही नहीं गया कि वह दिनभर या तो दुकान पर कपड़े फाड़ता है, शाम को सिल्लक मिलाता है और या फिर मटरगश्ती करने को निकल जाता है। इस बीच काकाजी पास के कस्बे से दो बोरी नाज की और पुरानी तराजू बाट भी ले आये थे। वह कपड़े नापता तो काकाजी नाज तोलते—हाथ बढ़े तो आमदनी भी बढ़नी चाहिए कि नहीं। फिर उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया। हाट-बाजार के दिन दुकान तो देखता ही था और दूसरे दिनों में गाँवभर में भटकने, मटरगश्ती करने और पीछे नदी के आसपास उगे झाड़-झंखाड़ों के बीच से बेर, जामुन, इमलियाँ बटोरने की आजादी तो थी ही। पहले जैसी। बस, चिट्ठियों पर मोहर ठोंकने में मस्त हो गया था....
दुकान और कोठारे के बीच एक भारी दरवाजा था जो हमेशा खुला रहता था। उसके एक पलड़े पर साँकल लटकी थी, दरवाजा बन्द करने के लिए नहीं, खटखटाने के लिए। बाई के लिए लगवा दी थी। पहले दरवाजे हिलते भी तो तीखी ‘चरर’ की आवाज होती और काकाजी को ‘खबर’ मिल जाती। उठते और रसोई घर की ओर चले जाते ‘खाना लग गया’। तब फर्श कच्चा था। काकाजी ने लाल पत्थर का मोटा फर्श लगवा लिया था। न अनगढ़ मेशन ने ध्यान दिया, न काकाजी ने मोटी फर्शियाँ इतनी ऊँची लग गयीं कि दरवाजे के बन्द होने की तो क्या हिलने की सँभावना भी खत्म हो गयी। तब, काकाजी ने मोटी, लोहे की साँकल लगवा दी।
तीसरे दिन बाई का ध्यान गया...एक बार नहीं, दो बार नहीं...तीन बार साँकल खड़खड़ाई, जोर-जोर से। बाई साँकल पकड़े दरवाजे की ओट में खड़ी रही।
खटखटाकर अन्दर रसोई में नहीं गयी।
काकाजी दुकान में नहीं थे।
‘क्यों रे...तू इसकूल नहीं गया ?’’ बाई ने गुस्से में पूछा और उसे ओसारे में आने का इशारा किया।
‘‘मास्टर ने मना कर दिया।’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘क्या मालूम।’’ उसने लापरवाही से कहा, ‘‘काकाजी को मालूम है।’’
बाई ओसारे में खड़ी उबली और रसोईघर तक उफनती चली गयी—‘‘भणेगो नहीं...कपड़ा फाड़ेगो....’’
दूसरे दिन काकाजी ने ओसारे में दरी बिछायी और उसके एक सिरे पर उसके सोने, बिछाने, ओढ़ने और पहनने के कपड़े रखे और दरी में लपेटकर लम्बी सुतली से कसकर बाँध दिया और बिस्तरबन्द को हाथ में उठाये उसे फाटे तक ले गये और धार जानेवाली बस में बैठा दिया, ‘‘सीधे घर जाना...किसी से भी वकील साब का घर पूछ लेना...ताँगा मत करना...।’’ उसकी हथेली में पाँच-पाँच के दो नोट और कुछ सिक्के रखे थे जो बस के किराये और स्कूल फीस के लिए थे। चाचाजी का घर था ही रहने-खाने के लिए। बिस्तरबन्द में पाजामा, कमीज की जोड़ी थी ही। एक नयी। कल शाम को ताबड़तोड़ बनवायी थी। दादा छुटपन से ही चाचाजी के यहाँ पढ़ रहे थे।
गाँव की दुनिया से निकल कुछ बड़ी दुनिया में घुसते ही जिन दो चीजों पर पहली बार नजर पड़ी वे थीं—‘ताँगे’ और पक्का ‘मोहन टॉकीज’। गाँव में ताँगे न ण्थे। वहीं थीं किराये की सायकल या साल दो साल में आने वाली नौटंकी। बहरहाल, वह एकान्तर घर से पूछता-पूछता शनि मन्दिर की गली में पहुँच गया। दादा बाहर ही खेल रहे थे। राहत की साँस ली।
उसे इतना ही मालूम था कि अब स्कूल नहीं, हाईस्कूल जाना है, आगे पढ़ने के लिए। किताबों से पहले दादा ने उसके नंगे पैरों को हवाई-चप्पलों में डाला और नाई के पास ले गये। नाई की दुकान देखकर चौंका। आइने के सामने कुर्सी पर बैठा था और कुर्सी के हत्थे कसकर पकड़ रखे थे। नाई बाल काटता जाता और कुर्सी के इर्द गिर्द घूमता जाता। उसे नहीं घूमना होता। बार-बार गाँव के रामप्रसाद काका का रौबीला चेहरा याद आता रहा : ‘‘सीधे बैठ..इधर घूम...उधर घूम...उधर झुक...।’’ बालों की लम्बाई रामप्रसाद काका की मर्जी और उसके बिना हिले-डुले, चीखे-चिल्लाए बाल कटते देखने की शक्ति पर निर्भर करती।
स्कूल का प्रवेश-फार्म दादा ने भरा, इसलिए स्कूल जाने के बाद मालूम पड़ा कि गणित में अच्छे नम्बरों के बावजूद उसे बायलॉजी पढ़ना है। समझ नहीं आया कि आखिर पढ़ना क्या पढ़ेगा। बायलॉजी की एक किताब देख राहत महसूस की अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित की तीन-तीन किताबों में सर फोड़ने के बजाय एक ही किताब से माथापच्ची करनी होगी और उसमें भी निर्जीव आँकड़ों और रेखाओं का जाल नहीं होगा। फूल होंगे, पत्तियाँ होंगी या मेंढक-मच्छर। गाँव की नदी के किनारे उगी झाड़ियों के जंगल से दूर हो जाने का गम कुछ तो कम हुआ।
आँकड़ों की दुनिया से छुटकारा तो मिला परन्तु पूरी तरह नहीं। दशहरा-दीवाली और गर्मियों की छुट्टियों में जब भी घर आता—दुकान के बही चौपड़ों से उलझना पड़ता। कुढ़न होती। सोचता, गर्मियों की छुट्टियाँ क्यों होती हैं...और होती हैं तो इतनी लम्बी क्यों...। काकाजी के साथ शाम को लालटेन की रोशनी में सिल्लक गिनते हुए पता नहीं कब वह अपने सपने देखने ही नहीं...गिनने भी लगा...वह स्कूल से निकल कॉलेज की सीढ़ियाँ चढ़ने को आतुर होता...काकाजी उसके, ‘इसकूल’ के सहपाठियों की तारीफ के पुल बाँधने लगते जो स्कूल की सीढ़ियाँ उतरते ही अपने खानदानी व्यवसाय में पीढ़ी-दर-पीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे थे। आमदनी वही हो, पर ‘कमा’ रहे थे।
अब उसे कोफ्त होती। स्कूल के साथी कामकाज में जुटे थे और मन मसोस कर ही उसे दुकान पर बैठना पड़ता, लट्ठा नापना पड़ता, साटन फाड़ना पड़ती। हिसाब लगा कर पैसे लेने-देने पड़ते। आँकड़े चुभते। बही चौपड़े लिखने में गड़बड़ी होती ही होती और काकाजी की डाँट सुननी ही पड़ती, ‘पता नहीं ‘हायस्कूल’ में क्या पढ़ाते हैं...इससे तो ‘इसकूल’ अच्छा था...बिस्तर बाँध यहीं आजा...भैया...’
‘इसकूल अच्छा था’ के आगे पापा कहते तो नहीं कि फीस भी नहीं लगती थी परन्तु लगता आर्थिक थकान आवाज में उतर आयी है।
वह कभी सोचता भी...हाईस्कूल और बस। बहुत पढ़ लिया।
दादा धार छोड़ कर इन्दौर चले गये। कॉलेज से भी बड़े कॉलेज पढ़ने यानी पी.जी. करने। वहाँ चचेरी बहन की ससुराल थी—यानी रहना फ्री, खाना फ्री। कपड़े तो यूँ भी लगते ही हैं—पढ़ो या न पढ़ो। दादा इन्दौर जा सकते हैं तो वह भी...
सपने बढ़ने लगे। गिनती करना मुश्किल ही नहीं, पीड़ादायक था। काकाजी की थकी आवाज कानों में भरी रहती और आँकड़ों में तो वह गलती करने लगा ही था।
ऐसे ही दुकान पर बैठे उसने काकाजी को बाई से कहते सुना, ‘‘बही-चौपड़े लिखना नहीं सीखेगा तो दुकान कैसे चलाएगा...बाद में।’’ काकाजी जानबूझकर नहीं कहते, ‘‘मेरे बाद में।’ बाई साड़ी का पल्लू आँखों पर रगड़ने लगती थी—
‘‘छुट्टी में आया है...सीखने में क्या हर्ज है...काम आएगा कभी न कभी।’’
बाई को भी लगता—सीखने की ही बात है...तो सीख लेने दे। चुपचाप रसोई में चली जाती।
घर में दो बुआएँ और दूर के मामा का लड़का भी रहता था। बही-खाते मिलाते हुए उसकी आँखें फटी की फटी रह गयीं, ‘इस छः बाय चार की दुकान की उससे भी कहीं छोटी, आमदनी में काकाजी पाँच लोगों का खर्च और उनकी पढ़ाई का खर्च कैसे चलाते होंगे...’
उसे लगा, उम्र और हिसाब दोनों में वह कच्चा है और पढ़-पढ़ कर आँखें भी कमजोर हो गयी हैं। बही-खातों में तो आँकड़े लिखे थे परन्तु एक बहुत पीड़ा-जनक राज़ बाई और काकाजी आँखों में छुपा था।
उस दिन बस का ड्राइवर अखबार के बण्डल के साथ काकाजी के नाम दादा की चिट्ठी भी फेंक गया। चिट्ठी कागज का खुला पुर्जा था। बड़े सोनीजी ने देखा तो अपने घर से ही जोरदार आवाज में चिट्ठी काकाजी को सुना दी, ‘‘मनु का मेडिकल में एडमीशन हो गया है...फार्म और फीस जल्दी भरना है। मनु को जल्दी से इन्दौर रवाना करना...। सब को ढोक !’’
उत्तेजना में वह बड़े सोनीजी के घर की तरफ भागा। चिट्ठी को जेब में रखा और अखबार के पन्ने टटोलने लगा। चयनित छात्रों में उसका नाम था। उसने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का फोटो भी नहीं देखा और देखते ही देखते वह गाँवभर का ‘डॉक्टर’ बन गया।
उसने सपने तो बहुत देखे थे...या देखे कम, गिने ज्यादा थे। याद नहीं आया कि यही सपना उसने देखा था। अब लग रहा था—यही उसका सपना था जो उसने कभी देखा ही नहीं था।
कुछ देर बाद काकाजी अखबार थामे भारी पैरों को घसीटते धीरे-धीरे चलते घर पहुँचे। माथे पर शिकनों का हुजूम लगा था।
एकाएक मुखर हो गयी बाई पड़ोसिनों से बधाई लेने में इतनी व्यस्त थी कि कब काकाजी रसोई में आकर, बिना चटाई बिछाए बैठ गये, पता नहीं चला। उस दिन काकाजी को रसोईघर की साँकल बजानी पड़ी। बाई ने थाली लगायी। काकाजी ने मुँह जूठा किया और उठ गए। कभी खाने की थाली में जूठन का एक दाना भी नहीं छोड़नेवाले काकाजी भरी थाली छोड़ दुकान में गये और खाली बही-खाते टटोलने लगे। अँतड़ियाँ कम, आँखें ज्यादा जल रही थीं।
कील से मन्दिर के दरवाजे की चाबी उतारी और चले गये।
अगले दो दिन सन्नाटे से भरे थे। कोई कुछ नहीं बोलता। बस दुकान में लट्ठे-साटन के फटने और रसोईघर में बर्तनों की उठापटक की आवाज होती। धीरे-धीरे फटने की आवाज रसोईघर तक पहुँचने लगी और उससे भी दुगनी रफ्तार से बर्तनों के पटकने की आवाज दुकान में भी सुनाई पड़ने लगी। काकाजी दमा के मरीज की तरह हवा पीते। गले में सूखी हवा भी फँस जाती और देर तक खाँसते रहते। आँखों में पानी आ जाता।
उन दिनों काकाजी ने उम्र के कई साल जी लिये। चेहरा झुर्रियों से अटा था, आँखें और धँस गयी थीं और गालों की हड्डियाँ चेहरे के रेगिस्तान में ढूहों सी उभरी थीं। आँखें खुलतीं तो खुली रहतीं, बन्द होतीं तो पलकों के अन्दर पुतलियाँ कंचे की गोलियों की तरह लुढ़कती रहतीं।
सन्नाटा टूटता नहीं। बाई के साँकल खड़खड़ाने की अवधि बढ़ती गयी। काकाजी हड़बड़ाकर उठते और खड़े रहते। भारी पैरों को उठा भी नहीं पाते..आगे बढ़ाने की बात तो दूर रही। बाई ओसारे में खड़ी साँकल झकझोरती रहती।
उससे तो काकाजी ने न कुछ कहा, न पूछा। बाई की आँखें जरूर बोलती सी लगतीं, तू फिकर मत कर रे...।
तीसरे दिन वह दुकान पर बैठा था। तभी काकाजी आते दिखे। अभी तो मन्दिर गये थे...? उसने घड़ी देखी—आठ ही बजे थे। दस से पहले तो काकाजी मन्दिर से नहीं आते ? अनायास ही उसने बही खोल ली।
काकाजी ने झुककर देहरी छुई, हथेली को माथे से लगाया, ‘‘रहने दे...जा, जल्दी से नहा-धो ले...खाना खा ले...दस बजे बस आती है, इन्दौर की...जल्दी कर...बस जल्दी भी आ जाती है।’’
अन्दर गया। बाई बिना नहाये-धोये, मन्दिर गये, फुलके सेंक रही थी यानी ‘पाप’ कर रही थी। चूल्हे से उठतीं लपटों में ‘पाप’ जल रहा था और बाई का चेहरा दिपदिपा रहा था।
ओसारे में काकाजी ने फिर दरी बिछायी और उसके बीच ओढ़ने, बिछाने की चीजें रख बिस्तरबन्द बनाया और कसकर बाँधा—सुतली से। फिर डाकघर गये—थोड़ा-सा लाख लाने के लिए। मुहर लगाने के लिए—अँगूठा था ही !
पहली बार की तरह, दूसरी बार भी मनु का, बिस्तरबन्ध बँधा—कभी-कभी ही मुँह खोलनेवाली बाई के ‘कहने’ पर।
कब बस ने गुजरी की सीमा पार की और कब राष्ट्रीय राजमार्ग ‘ए.बी.’ रोड पर दौड़ती-हाँफती, हिचकोले खाती इन्दौर की शहर-सीमा में घुसी, पता ही नहीं चला। बस खचाखच सवारियों से भरी थी और मनु बीच-रास्ते में बिस्तरबन्द पर बैठा, जैसे-तैसे अपने को गिरने लुढ़कने से बचाते हुए। बाहर का कुछ नजर नहीं आ रहा था। सारे रास्ते बस के फर्श पर आड़े-तिरछे खड़े पैरों, जूतों और हवाई चप्पलों को देखता रहा। किसी का ध्यान मनु की ओर था ही नहीं—यहाँ तक कि खुद मनु का। मनु के पैर ही नहीं, वह खुद भी ‘हवाई-चप्पलों’ में सफर कर रहा था। बस स्टैण्ड पर पहुँच गयी और उसे पता ही नहीं चला कि कब वह बिस्तरबन्द पर अधलेटा मेडिकल कॉलेज के सामने से गुजर गया।
पहले दिन मनु कॉलेज जा नहीं पाया। कपड़े नहीं थे। कपड़े यानी प्रथम वर्ष, मेडिकल स्टूडेंट का गणवेश। बिस्तरबन्द में वे ही कपड़े काकाजी ने बाँध दिये थे जिन्हें पहनकर वह स्कूल भी गया था और एक साल कॉलेज भी। रंगीन धारीदार कमीज की जोड़ी और सफेद पापलीन के पायजामे। कमीज सफेद झक्क चाहिए थी—लेकिन रंगीन थी और ऊपर से धारीदार। पायजामे सफेद थे—चाहिए पैंट थे। जूते-मोजे तो रेडीमेड मिल गये परन्तु पैंट-शर्ट सिलने को टेलर को दिये थे। दुकान का साप्ताहिक अवकाश था। गया और आ गया। दादा ‘डरना नहीं’ कहकर बहुत पहले ही कॉलेज चले गये थे और वह अधखुले बिस्तरबन्द पर बैठा ‘क्या करे’ सोचता रहा। कमीज-पायजामे में तो कॉलेज जा नहीं सकता था। दादा का कहना था !
नहाकर भी क्या करेगा...सोच, बहुत देर तक नहाना स्थगित करता रहा। बिस्तरबन्द टटोलता रहा—टॉवेल था ही नहीं। ‘चन्दू’ (काकाजी को चन्दू ही कहकर बुलाते थे) के पास होगा ही...। एक टॉवेल से दो बदन क्यों नहीं पोंछे जा सकते, यही सोच काकाजी ने बिस्तरबन्द में नया टॉवेल नहीं रखा होगा—मनु ने सोचा।
कपड़े होते हुए भी, ड्रेस नहीं है। ड्रेस नहीं, इसलिए कॉलेज नहीं जा सकता—अजीब लग रहा था मनु को। यह भी कोई बात हुई ? कोई नंगा तो नहीं जाता ! या कमीज पायजामा पहनकर जाने से—कॉलेज ‘नंगा’ हो जाता ? स्कूल तो नहीं हुआ, और धार में एक साल कॉलेज में भी कमीज-पायजामे में ही गया—वह भी पैरों में हवाई-चप्पल पहने। न मनु हवाई-चप्पल पहन उड़ा, न स्कूल-कॉलेज की बिल्डिंग जमीन में धँसी। पता नहीं, कैसे ईंट-चूने से बनी थी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और कैसी थीं कॉलेज की दीवारें ! सफेद ? पता नहीं। बस में सीट पर बैठा होता तो शायद दीख जाती। कॉलेज के पहले दिन ही—तड़ी।
कल शाम को दादा दो सीनियर्स को मिलाने लाये थे।
‘‘तो यह है नया पंक्षी।’’ दोनों ने एक साथ चहकते हुए उसका अभिवादन का जवाब मनु की पीठ पर ‘धौल’ जमाते हुए दिया था।
मनु ने दादा की ओर देखा। ‘पंक्षी ? कौन ? मनु ने दोनों बाँहों की जगह टटोला—
‘‘देख क्या रहा है...पैर छू...सीनियर्स हैं।’’ दादा खुद सीनियर्स बन आदेश दे रहे थे।
मनु को सिर, गरदन, पीठ और हाथ झुकाने पड़े। न जान-पहचान, न आदर-सम्मान फिर भी...?
‘‘वेल, बी.सी. (दादा का नाम), पंक्षी की ट्रेनिंग शुरू कर दी...’’ एक सीनियर जिसके हाथ में मोटी-सी किताब थी, कु्र्सी पर बैठते हुए बोला।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i