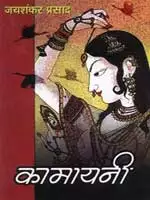|
कविता संग्रह >> कामायनी कामायनीजयशंकर प्रसाद
|
271 पाठक हैं |
||||||||
जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
जिस समय खड़ी बोली और आधुनिक हिन्दी साहित्य
किशोरावस्था में पदार्पण कर रहे थे। काशी के ‘सुंघनी साहु’ के प्रसिद्ध घराने में
श्री जयशंकर प्रसाद का संवत् 1946 में जन्म हुआ। व्यापार में कुशल और
साहित्य सेवी – आपके पिता श्री देवी प्रसाद पर लक्ष्मी की कृपा
थी। इस तरह का प्रसाद का पालन पोषण लक्ष्मी औऱ सरस्वती के कृपापात्र घराने
में हुआ। प्रसाद जी का बचपन अत्यन्त सुख के साथ व्यतीत हुआ। आपने अपनी
माता के साथ अनेक तीर्थों की यात्राएँ की। पिता और माता के दिवंगत होने पर
प्रसाद जी को अपनी कॉलेज की पढ़ाई रोक देनी पड़ी और घर पर ही बड़े भाई
श्री शम्भुरत्न द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था की गई। आपकी सत्रह वर्ष की आयु
में ही बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। फिर प्रसाद जी ने पारिवारिक क्षण
मुक्ति के लिए सम्पत्ति का कुछ भाग बेचा। इस प्रकार आर्थिक सम्पन्नता और
कठिनता के किनारों में झूलता प्रसाद का लेखकीय व्यक्तित्व समृद्धि पाता
गया। संवत् 1984 में आपने पार्थिव शरीर त्यागकर परलोक गमन किया।
आमुख
आर्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु का
इतिहास से
लेकर पुराण और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। श्रद्धा और मनु के सहयोग
से मानवता के विकास की कथा को, रूपक के आवरण में, चाहे पिछले काल में मान
लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ
निरूक्त के द्वारा किया गया, किन्तु मन्वंतर के अर्थात् मानवता के नवयुग
के प्रवर्तक के रूप में मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। प्रायः
लोक गाथा और इतिहास में मिथ्या और सत्य को व्यवधान मानते हैं। किन्तु सत्य
मिथ्या से अधिक विचित्र होता है। आदिम युग के मनुष्यों के प्रत्येक दल ने
ज्ञानोन्मेषक अरुणोदय में जो भावपूर्ण इतिवृत्त संग्रहीत किए थे, उन्हें
आज गाथा या पौराणिक उपाख्यान कहकर अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उन
चरित्रों के साथ भावनाओं का भी बीच-बीच में संबंध लगा हुआ-सा दीखता है।
घटनाएं कहीं-कहीं अतिरंजित-सी भी जान पड़ती हैं। तथ्य-संग्रहकारिणी
तर्कबुद्धि को ऐसी घटनाओं में रूपक का आरोप कर लेने की सुविधा हो जाती है।
किंतु उनमें भी कुछ सत्यांश घटना से संबद्ध है ऐसा तो मानना ही पड़ेगा। आज
के मनुष्य के समीप तो उसकी वर्तमान संस्कृति का क्रमपूर्ण इतिहास ही होता
है; परंतु उसके इतिहास की सीमा जहां से प्रारंभ होती है ठीक उसी के पहले
सामूहिक चेतना की दृढ़ और गहरे रंगों की रेखाओं से, बीती हुई और भी पहले
की बातों का उल्लेख स्मृति-पट पर अमिट रहता है; परंतु कुछ अतिरंजित-सा। वे
घटनाएं आज विचित्रता से पूर्ण जान पड़ती हैं। संभवतः इसीलिए हमको अपनी
प्राचीन श्रुतियों का निरुक्त के द्वारा अर्थ करना पड़ा; जिससे कि उन
अर्थों का अपनी वर्तमान रुचि से सामजंस्य किया जाए।
यदि श्रद्धा और मनु अर्थात् मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। आज हम सत्य का अर्थ घटना कर लेते हैं। तब भी, उसके तिथिक्रम मात्र से संतुष्ट होकर, मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा इतिहास की घटना के भीतर कुछ देखना चाहते हैं। उसके मूल में क्या रहस्य है ? आत्मा की अनुभूति! हां, उसी भाव के रूप-ग्रहण की चेष्टा सत्य या घटना बनकर प्रत्यक्ष होती है। फिर, वे सत्य घटनाएं स्थूल और क्षणिक होकर मिथ्या और अभाव में परिणत हो जाती हैं। किन्तु सूक्ष्म अनुभूति या भाव, चिरंतर सत्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, जिसके द्वारा युग-युग के पुरुषों की और पुरुषार्थों की अभिव्यक्ति होती रहती है।
जल-प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है, जिसने मनु को देवों से विलक्षण, मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। ‘मनवे वै प्रातः’ इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के आठवें अध्याय में मिलता है। देवगण के उच्छृंखल स्वभाव, निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात् श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को नए युग की सूचना मिली। इस मन्वंतर के प्रवर्त्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धादेव कहा गया है, ‘श्रद्धादेवी वै मनु, (का.1 प्र.1)’। भागवत में इन्हीं वैवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारम्भ माना गया है।
यदि श्रद्धा और मनु अर्थात् मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। आज हम सत्य का अर्थ घटना कर लेते हैं। तब भी, उसके तिथिक्रम मात्र से संतुष्ट होकर, मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा इतिहास की घटना के भीतर कुछ देखना चाहते हैं। उसके मूल में क्या रहस्य है ? आत्मा की अनुभूति! हां, उसी भाव के रूप-ग्रहण की चेष्टा सत्य या घटना बनकर प्रत्यक्ष होती है। फिर, वे सत्य घटनाएं स्थूल और क्षणिक होकर मिथ्या और अभाव में परिणत हो जाती हैं। किन्तु सूक्ष्म अनुभूति या भाव, चिरंतर सत्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, जिसके द्वारा युग-युग के पुरुषों की और पुरुषार्थों की अभिव्यक्ति होती रहती है।
जल-प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है, जिसने मनु को देवों से विलक्षण, मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। ‘मनवे वै प्रातः’ इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के आठवें अध्याय में मिलता है। देवगण के उच्छृंखल स्वभाव, निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात् श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को नए युग की सूचना मिली। इस मन्वंतर के प्रवर्त्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धादेव कहा गया है, ‘श्रद्धादेवी वै मनु, (का.1 प्र.1)’। भागवत में इन्हीं वैवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारम्भ माना गया है।
‘‘ततो मनुः
श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत
श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रानुस आत्मवान्’’ (9-1-11)
श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रानुस आत्मवान्’’ (9-1-11)
छांदोग्य उपनिषद् में मनु और श्रद्धा की
भावसूचक व्याख्या
भी मिलती है। ‘यदावै श्रद्धधाति अथ मनुते नाऽश्रद्धधन्
मनुते’
यह कुछ निरुक्त की-सी व्याख्या है। ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का
नाम ऋषियों की तरह मिलता है। श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का
परिचय देते हुए लिखा है, ‘काम-गोत्रजा
श्रद्धानपामर्षिका’।
श्रद्धा कामगोत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी
कहा जाता है। मनु प्रथम पथ-प्रदर्शक और अग्निहोत्र प्रज्वलित करने वाले
तथा अन्य कई वैदिक कथाओं के नायक हैं:-‘मनुर्हवा अग्रे
यज्ञेनेजे
यदनुकृत्येमा: प्रजा यजन्ते’ (5-1 शतपथ)। इनके संबंध में वैदिक
साहित्य में बहुत-सी बातें बिखरी हुई मिलती हैं; किंतु उनका क्रम स्पष्ट
नहीं है। जल-प्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के आठवें अध्याय
से आरम्भ होता है, जिसमें उनकी नाव के उत्तरगिरि हिमवान प्रदेश में
पहुंचने का प्रसंग है। वहां ओध के जल का आवरण होने पर मनु भी जिस स्थान पर
उतरे उसे मनोरवसर्पण कहते हैं। अपीपरं वै त्वा, वृक्षे नावं
प्रतिबध्नीष्व, तं तु त्वा मा गिरौ सन्त मुदकमन्तश्चैत्सीद् यावद्
यावदुदकं समवायात्-तावत्-तावदन्व-वसर्पासि इति स ह तावत्
तावदेवान्ववससर्प। तदप्येतदुत्तरस्य गिरेर्मनोरवसर्पण-मिति। (8-1)
श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरंभ करने का प्रयत्न हुआ। किन्तु असुर पुरोहित के मिल जाने से इन्होंने पशु-बलि की-‘किलाताकुली-इति हासुर ब्रह्मावासतु:। तौ होचतु:-श्रद्धादेवो वै मनु:-आवं नु वेदावेति। तौ हागत्योचतु:मनो। बाजयाब त्वेति।’
इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व-परिचित-देव-प्रवृत्ति जाग उठी-उसने इड़ा के संपर्क में आने पर उन्हें श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरी ओर प्रेरित किया। इड़ा के संबंध में शतपथ में कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई और उस पूर्णयोषिता को देखकर मनु ने पूछा कि ‘‘तुम कौन हो ?’’ इड़ा ने कहा,‘तुम्हारी दुहिता हूं।’ मनु ने पूछा कि ‘मेरी दुहिता कैसे ?’ उसने कहा, ‘तुम्हारे दही, घी इत्यादि के हवियों से ही मेरा पोषण हुआ है।’ ‘तां ह’ मनुरुवाच-‘का असि’ इति, ‘तव दुहिता’ इति। ‘कथं भगवति ? मम दुहिता’ इति। (शतपथ 6 प्र.3 ब्रा.)
इड़ा के लिए मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ और श्रद्धा से वे कुछ खिंचे। ऋग्वेद में इड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है। यह प्रजापति मनु की पथ-प्रदर्शिता मनुष्यों का शासन करने वाली कही गयी है। ‘‘इड़ामकृण्वपन्मनुषस्य शासनीम्’’ (1-31-11 ऋग्वेद)। इड़ा के संबंध में ऋग्वेद में कई मंत्र मिलते हैं। ‘‘सरस्वती साधयंती धियं न इड़ा देवी भारती विश्वमूर्ति: तिस्त्रो देवी: स्वघयावर्हिरेदमच्छिंद्र पान्तु शरणं निषदय।’’ (ऋग्वेद 2-3-8) ‘‘ आनो यज्ञं भारती तूयं मेत्विड़ा मनुष्यवदिह चेतयंती। तिस्त्रो देवीर्वहिरेदं स्योनं सरस्वती स्वपस: सदंतु। (10-110-8) इन मंत्रों में मध्यमा, वैखरी और पश्यंती की प्रतिनिधि भारती, सरस्वती के साथ इड़ा का नाम आया है। लौकिक संस्कृति में इड़ा शब्द पृथ्वी अर्थात् बुद्धि, वाणी आदि का पर्यायवाची है।-‘‘गो भू र्वाचात्स्विड़ा इला’’-(अमर)। इस इड़ा या वाक् के साथ मनु या मन के एक और विवाद का भी शतपथ में उल्लेख मिलता है जिसमें दोनों अपने महत्व के’’ लिए झगड़ती हैं ‘अथतोमनसश्च’ (4 अध्याय 5 ब्राह्मण)। ऋग्वेद में इड़ा को घी ?, बुद्धि का साधन करने वाली; मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली कहा है। पिछले काल में संभवतः इड़ा को पृथ्वी आदि से सम्बद्ध कर दिया गया हो, किन्तु ऋग्वेद 5-5-8 में इड़ा और सरस्वती के साथ मही का अलग उल्लेख स्पष्ट है। ‘‘इड़ा सरस्वती मही तिस्त्रोदेवी मयोभुव:’’ से मालूम पड़ता है कि मही से इड़ा भिन्न है। इड़ा को मेघसवाहिनी नाड़ी भी कहा गया है।
अनुमान किया जा सकता है बुद्धि का विकास, राज्य-स्थापना इत्यादि इड़ा के प्रभाव से ही मनु ने किया। फिर तो इड़ा पर भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगण का कोपभाजन होना पड़ा। ‘तद्वै देवानां आग आस’ (7-4 शतपथ)। इड़ा देवताओं की स्वसा थी। मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली थी। इसलिए यज्ञों में इड़ा का बुद्धिवाद् श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है। फिर बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में, दुख मिलना स्वाभाविक है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, साकेंतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात् मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमश: श्रद्धा और इड़ा से भी सरलता से लगाया जाता है। ‘श्रद्धा हृदय याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ! (ऋग्वेद 10-151-4) इन्हीं सबके आधार पर ‘कामायनी’ की कथा-सृष्टि हुई है। हां, ‘कामायनी’ की कथा श्रृंखला मिलाने के लिए कहीं-कहीं थोड़ी-बहुत कल्पना को भी काम में ले लाने का अधिकार मैं नहीं छोड़ सका हूं।
श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरंभ करने का प्रयत्न हुआ। किन्तु असुर पुरोहित के मिल जाने से इन्होंने पशु-बलि की-‘किलाताकुली-इति हासुर ब्रह्मावासतु:। तौ होचतु:-श्रद्धादेवो वै मनु:-आवं नु वेदावेति। तौ हागत्योचतु:मनो। बाजयाब त्वेति।’
इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व-परिचित-देव-प्रवृत्ति जाग उठी-उसने इड़ा के संपर्क में आने पर उन्हें श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरी ओर प्रेरित किया। इड़ा के संबंध में शतपथ में कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई और उस पूर्णयोषिता को देखकर मनु ने पूछा कि ‘‘तुम कौन हो ?’’ इड़ा ने कहा,‘तुम्हारी दुहिता हूं।’ मनु ने पूछा कि ‘मेरी दुहिता कैसे ?’ उसने कहा, ‘तुम्हारे दही, घी इत्यादि के हवियों से ही मेरा पोषण हुआ है।’ ‘तां ह’ मनुरुवाच-‘का असि’ इति, ‘तव दुहिता’ इति। ‘कथं भगवति ? मम दुहिता’ इति। (शतपथ 6 प्र.3 ब्रा.)
इड़ा के लिए मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ और श्रद्धा से वे कुछ खिंचे। ऋग्वेद में इड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है। यह प्रजापति मनु की पथ-प्रदर्शिता मनुष्यों का शासन करने वाली कही गयी है। ‘‘इड़ामकृण्वपन्मनुषस्य शासनीम्’’ (1-31-11 ऋग्वेद)। इड़ा के संबंध में ऋग्वेद में कई मंत्र मिलते हैं। ‘‘सरस्वती साधयंती धियं न इड़ा देवी भारती विश्वमूर्ति: तिस्त्रो देवी: स्वघयावर्हिरेदमच्छिंद्र पान्तु शरणं निषदय।’’ (ऋग्वेद 2-3-8) ‘‘ आनो यज्ञं भारती तूयं मेत्विड़ा मनुष्यवदिह चेतयंती। तिस्त्रो देवीर्वहिरेदं स्योनं सरस्वती स्वपस: सदंतु। (10-110-8) इन मंत्रों में मध्यमा, वैखरी और पश्यंती की प्रतिनिधि भारती, सरस्वती के साथ इड़ा का नाम आया है। लौकिक संस्कृति में इड़ा शब्द पृथ्वी अर्थात् बुद्धि, वाणी आदि का पर्यायवाची है।-‘‘गो भू र्वाचात्स्विड़ा इला’’-(अमर)। इस इड़ा या वाक् के साथ मनु या मन के एक और विवाद का भी शतपथ में उल्लेख मिलता है जिसमें दोनों अपने महत्व के’’ लिए झगड़ती हैं ‘अथतोमनसश्च’ (4 अध्याय 5 ब्राह्मण)। ऋग्वेद में इड़ा को घी ?, बुद्धि का साधन करने वाली; मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली कहा है। पिछले काल में संभवतः इड़ा को पृथ्वी आदि से सम्बद्ध कर दिया गया हो, किन्तु ऋग्वेद 5-5-8 में इड़ा और सरस्वती के साथ मही का अलग उल्लेख स्पष्ट है। ‘‘इड़ा सरस्वती मही तिस्त्रोदेवी मयोभुव:’’ से मालूम पड़ता है कि मही से इड़ा भिन्न है। इड़ा को मेघसवाहिनी नाड़ी भी कहा गया है।
अनुमान किया जा सकता है बुद्धि का विकास, राज्य-स्थापना इत्यादि इड़ा के प्रभाव से ही मनु ने किया। फिर तो इड़ा पर भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगण का कोपभाजन होना पड़ा। ‘तद्वै देवानां आग आस’ (7-4 शतपथ)। इड़ा देवताओं की स्वसा थी। मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली थी। इसलिए यज्ञों में इड़ा का बुद्धिवाद् श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है। फिर बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में, दुख मिलना स्वाभाविक है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, साकेंतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात् मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमश: श्रद्धा और इड़ा से भी सरलता से लगाया जाता है। ‘श्रद्धा हृदय याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ! (ऋग्वेद 10-151-4) इन्हीं सबके आधार पर ‘कामायनी’ की कथा-सृष्टि हुई है। हां, ‘कामायनी’ की कथा श्रृंखला मिलाने के लिए कहीं-कहीं थोड़ी-बहुत कल्पना को भी काम में ले लाने का अधिकार मैं नहीं छोड़ सका हूं।
जयशंकर प्रसाद
चिंता
हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, बैठ शिला की
शीतल छाँह,
एक पुरुष, भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह।
नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन,
एक तत्त्व की ही प्रधानता-कहो उसे जड़ या चेतन।
दूर-दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय-समान,
नीरवता-सी शिला-चरण से टकराता फिरता पवमान।
तरुण तपस्वी-सा वह बैठा साधन करता सुर-स्मशान,
नीचे प्रलयसिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान।
उसी तपस्वी-से लम्बे थे देवदारु दो चार खड़े,
हुए हिम-धवल, जैसे पत्थर बन कर ठिठुरे रहे अड़े।
अवयव की दृढ़ मांस-पेशियां, ऊर्जस्वित था वीर्य्य अपार,
स्फीत शिरायें, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार।
चिंता-कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओत-प्रोत,
उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत।
बंधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही,
उतर चला था वह चल-प्लावन, और निकलने लगी मही।
निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी,
वहां अकेली प्रकृति सुन रही, हंसती-सी पहचानी-सी।
‘‘ओ चिंता की पहली रेखा, अरी विश्व-वन की व्याली,
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कम्प-सी मतवाली।
हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खललेखा,
हरी-भरी-सी दौड़-धूप, ओ जल-माया की चल-रेखा।
इस ग्रहकक्षा की हलचल-री तरल गरल लघु-लहरी,
जरा अमर-जीवन की, और न कुछ सुनने वाली, बहरी।
अरी व्याधि की सूत्र-धारिणी-अरी आधि, मधुमय अभिशाप,
हृदय-गगन में धूमकेतु-सी, पुण्ड-सृष्टि में सुन्दर पाप।
मनन करावेगी तू कितना ? निश्चिंत जाति का जीव-
अमर मरेगा क्या ? तू कितनी डाल रही है नींव।
आह ! घिरेगी हृदय-लहलहे-खेतों पर करका-घन-सी,
छिपी रहेगी अंतरतम में सब के तू निगूढ़ धन-सी।
बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम !
अरी पाप है तू, जा, चल जा यहां नहीं कुछ तेरा काम।
विस्मृत आ, अवसाद घेर ले, नीरवते ! बस चुप कर दे,
चेतनता चल जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे।’’
‘‘चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की,
उतनी ही अनंनत में बनती जातीं रेखायें दुख की।
आह सर्ग के अग्रदूत ! तुम असफल हुए, विलीन हुए,
भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए।
अरी आंधियो ! ओ बिजली की दिवा-रात्रि तेरा नर्तन,
उसी वासना की उपासना, वह तेरा प्रत्यावर्त्तन।
मणि-दीपों के अंधकारमय अरे निराशा पूर्ण भविष्य !
देव-दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष्य।
अरे अमरता के चमकीले पुतलो ! तेरे वे जयनाद-
कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बन कर मानो दीन विषाद।
प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब थे भूले मद में,
भोले थे, हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में।
वे सब डूबे, डूबा उनका विभव, बन गया पारावार-
उमड़ रहा था देव-सुखों पर दुःख-जलाधि का नाद अपार।’’
‘‘वह उन्मत्त विलास हुआ क्या ! स्वप्न रहा या छलना थी !
देवसृष्टि की सुख-विभावरी ताराओं की कलना थी।
चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास,
कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख-विश्वास।
सुख, केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना,
छायापथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना।
सब कुछ थे स्वायत्त, विश्व के-बल, वैभव, आनंद अपार,
उद्वेलित, लहरों-सा होता उस समृद्धि का सुख-संचार।
कीर्त्ति, दीप्ति, शोभा थी नचती अरुण-किरणों-सी चारों ओर,
सप्तसिंधु के तरल कणों में, द्रुम-दल में, आनंद-विभोर।
शक्ति रही हां शक्ति-प्रकृति थी पद-तल में विनम्र विश्रांत,
कंपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत।
स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न विश्रृंखल होती सृष्टि ?
अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि।
गया, सभी कुछ गया, मधुर तम सुर-बालाओं का श्रृंगार,
उषा ज्योत्स्ना-सा यौवन-स्मित मधुप-सदृश निश्चिंत विहार।
भरी वासना-सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह,
प्रलय-जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा कराह।’
‘‘चिर-किशोर-वय, नित्यविलासी-सुरभित जिससे रहा दिगंत
आज तिरोहित हुआ कहां वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत ?
कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमलिंगन हुए विलीन,
मौन हुई है मूर्च्छित तानें और न सुन पड़ती अब बीन।
अब न कपोलों पर छाया-सी पड़ती मुख की सुरभित भाप,
भुज-भूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप।
कंकण क्वणित, रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार,
मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय को होता अभिसार।
सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक-अधीर,
सब में एक अचेतन गति थी, जिससे पिछड़ा रहे समीर।
वह अनंग-पीड़ा-अनुभव-सा अंग-भगियों का नर्तन,
मधुकर के मरंद-उत्सव-सा मदिर भाव से आवर्तन।
सुरा सुरभिमय बदन अरुण से नयन भरे आलस अनुराग,
कल कपोल था जहॉ बिछलता कल्पवृक्ष का पीत पराग।
विकल वासना के प्रतिनिधि से सब मुरझाये चले गये,
आह ! जले अपनी ज्वाला से सिर वे जल में गले, गये।’’
‘‘अरी अपेक्षा-भरी अमरते ! री अतृप्ति ! निर्बाध विलास !
द्विधा-रहित अपलक नयनों की भूख-भरी दर्शन की प्यास।
बिछुड़े सब तेरे आलिंगन, पुलक-स्पर्श का पता नहीं,
मधुमय चुंबन कातरतायें, आज न मुख को सता रहीं।
रत्न-सौध के वातायन- जिसमें आता मधु-मन्दर समीर,
टकराती होगी अब उनमें तिमिंगिलों की भीड़ अधीर।
देवकामिनी के नयनों से जहां नील नलिनों की सृष्टि-
होती थी, अब वहां हो रही प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि।
वे अम्लान-कुसुम-सुरभित-मणि-रचित मनोहर मालायें,
बनी श्रृंखला, जकड़ीं जिनमें विलासिनी सुर-बालायें।
देव-यजन के पशुयज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला,
जलनिधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला।’’
‘‘उनको देख कौन रोया यों अंतरिक्ष में बैठ अधीर !
व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय यह प्रालेय हलाहल नीर !
हाहाकार हुआ क्रंदनमय कठिन कुलिश होते थे चूर,
हुए दिगंत बधिर, भीषण रव बार-बार होता था क्रूर।
दिग्दाहों से घूम उठे, या जलधर उठे क्षितिज-तट के !
सघन गगन में भीमप्रकंपन, झंझा के चलते भटके।
अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई,
वरुण व्यस्त थे, घनी कालिमा स्तर-स्तर जमती पीन हुई।
पंचभूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के शकल-निपात
उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रहीं ज्यों खोया प्रात।
बार-बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष,
मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष।
उधर गरजतीं सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी,
चली आ रहीं फेन उगलती फन फैलाये व्यालों-सी।
धंसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वाला-मुखियों के निश्वास
और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास।
सबल तरंगाघातों से उस क्रुद्ध सिंधु के, विचलित-सी-
व्यस्त महाकच्छप-सी धरणी ऊभ-चूभ थी विकलित-सी।
बढ़ने लगा विलास-वेग-सा वह अतिभैरव जल-संधात,
तरल-तिमिर से प्रलय-पवन का होता आलिंगन, प्रतिघात।
बेला क्षण-क्षण निकट आ रही क्षितिज क्षीण, फिर लीन हुआ,
उदधि डुबाकर अखिल धारा को बस मर्यादा-हीन हुआ !
पंचभूत का यह तांडवमय नृत्य हो रहा था कब का।’’
‘‘एक नाव थी, और न उसमें डांड़े लगते, या पतवार,
तरल तरंगों में उठ-गिरकर बहती पगली बारंबार।
लगते प्रबल थपेड़े धुधले तट का था कुछ पता नहीं,
कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वहीं।
लहरें व्योम चूमती उठतीं, चपलायें असंख्य नचतीं,
गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदें निज संसृति रचतीं।
चपलायें उस जलधि-विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थीं,
ज्यों विराट बाड़व-ज्वालायें खंड-खंड हो रोती थीं।
जलनिधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते,
हुआ विलोड़ित गृह, तब प्राणी कौन! कहॉ! कब ! सुख पाते ?
घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध,
और चेतना थी विलखाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध।
उस विराट् आलोड़न में ग्रह, तारा बुद-बुद से लगते,
प्रखर प्रलय-पावस में जगमग, ज्योतिरिंगणों-से जलते।
प्रहर दिवस कितने बीते, अब इसको कौन बता सकता,
इनके सूचक उपकरणों को चिह्न न कोई पा सकता।
काला शासन-चक्र मृत्यु का कब तब चला, न स्मरण रहा,
महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा।
किंतु, उसी न ला टकराया इस उत्तरगिरि के शिर से,
देव-सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से।
आज अमरता का जीवित हूं मैं वह भीषण जर्जर दंभ,
आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम-पात्र मय सा विष्कंभ।’’
‘‘ओ जीवन की सरु-मीरीचिका, कायरता के अलस विषाद !
अरे पुरातन अमृत ! अगतिमय मोहमुग्ध जर्जर अवसाद !
मौन ! नाश ! विध्वंस ! अंधेरा ! शून्य बना जो प्रकट अभाव,
वहीं सत्य है, अरी अमरते ! तुझको ! यहां कहां अब ठांव।
मृत्यु, अरी चिर-निद्रे ! तेरा अंक हिमानी-सा शीतल,
तू अनंत में लहर बनाती काल-जलधि की-सी हलचल।
महानृत्य का विषम सम अरी अखिल स्पंदनों की तू माप,
तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप।
अंधकार के अट्टहास-सी मुखरित सतत चिरंतन सत्य,
छिपी सृष्टि के कण-कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य।
जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नीन धन-माला में,
सौदामिनी-संधि-सा सुन्दर क्षण भर रहा उजाला में।’’
पवन पी रहा था शब्दों को निर्जनता की उखड़ी सांस,
टकराती थी, दीन प्रतिध्वनि बनी हिम-शिलाओं के पास।
धू-धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य,
आकर्षण-विहीन विद्युत्कण बने भारवाही थे भृत्य।
मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती ती दृष्टि,
परमव्योम से भौतिक कण-सी घने कुहासों की थी वृष्टि।
वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल-संघात,
सौरचक्र में आवर्त्तन था प्रलय निशा का होता प्रात !
 गूगल प्ले स्टोर पर पढ़ें
गूगल प्ले स्टोर पर पढ़ें
एक पुरुष, भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह।
नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन,
एक तत्त्व की ही प्रधानता-कहो उसे जड़ या चेतन।
दूर-दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय-समान,
नीरवता-सी शिला-चरण से टकराता फिरता पवमान।
तरुण तपस्वी-सा वह बैठा साधन करता सुर-स्मशान,
नीचे प्रलयसिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान।
उसी तपस्वी-से लम्बे थे देवदारु दो चार खड़े,
हुए हिम-धवल, जैसे पत्थर बन कर ठिठुरे रहे अड़े।
अवयव की दृढ़ मांस-पेशियां, ऊर्जस्वित था वीर्य्य अपार,
स्फीत शिरायें, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार।
चिंता-कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओत-प्रोत,
उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत।
बंधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही,
उतर चला था वह चल-प्लावन, और निकलने लगी मही।
निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी,
वहां अकेली प्रकृति सुन रही, हंसती-सी पहचानी-सी।
‘‘ओ चिंता की पहली रेखा, अरी विश्व-वन की व्याली,
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कम्प-सी मतवाली।
हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खललेखा,
हरी-भरी-सी दौड़-धूप, ओ जल-माया की चल-रेखा।
इस ग्रहकक्षा की हलचल-री तरल गरल लघु-लहरी,
जरा अमर-जीवन की, और न कुछ सुनने वाली, बहरी।
अरी व्याधि की सूत्र-धारिणी-अरी आधि, मधुमय अभिशाप,
हृदय-गगन में धूमकेतु-सी, पुण्ड-सृष्टि में सुन्दर पाप।
मनन करावेगी तू कितना ? निश्चिंत जाति का जीव-
अमर मरेगा क्या ? तू कितनी डाल रही है नींव।
आह ! घिरेगी हृदय-लहलहे-खेतों पर करका-घन-सी,
छिपी रहेगी अंतरतम में सब के तू निगूढ़ धन-सी।
बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम !
अरी पाप है तू, जा, चल जा यहां नहीं कुछ तेरा काम।
विस्मृत आ, अवसाद घेर ले, नीरवते ! बस चुप कर दे,
चेतनता चल जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे।’’
‘‘चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की,
उतनी ही अनंनत में बनती जातीं रेखायें दुख की।
आह सर्ग के अग्रदूत ! तुम असफल हुए, विलीन हुए,
भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए।
अरी आंधियो ! ओ बिजली की दिवा-रात्रि तेरा नर्तन,
उसी वासना की उपासना, वह तेरा प्रत्यावर्त्तन।
मणि-दीपों के अंधकारमय अरे निराशा पूर्ण भविष्य !
देव-दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष्य।
अरे अमरता के चमकीले पुतलो ! तेरे वे जयनाद-
कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बन कर मानो दीन विषाद।
प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब थे भूले मद में,
भोले थे, हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में।
वे सब डूबे, डूबा उनका विभव, बन गया पारावार-
उमड़ रहा था देव-सुखों पर दुःख-जलाधि का नाद अपार।’’
‘‘वह उन्मत्त विलास हुआ क्या ! स्वप्न रहा या छलना थी !
देवसृष्टि की सुख-विभावरी ताराओं की कलना थी।
चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास,
कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख-विश्वास।
सुख, केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना,
छायापथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना।
सब कुछ थे स्वायत्त, विश्व के-बल, वैभव, आनंद अपार,
उद्वेलित, लहरों-सा होता उस समृद्धि का सुख-संचार।
कीर्त्ति, दीप्ति, शोभा थी नचती अरुण-किरणों-सी चारों ओर,
सप्तसिंधु के तरल कणों में, द्रुम-दल में, आनंद-विभोर।
शक्ति रही हां शक्ति-प्रकृति थी पद-तल में विनम्र विश्रांत,
कंपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत।
स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न विश्रृंखल होती सृष्टि ?
अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि।
गया, सभी कुछ गया, मधुर तम सुर-बालाओं का श्रृंगार,
उषा ज्योत्स्ना-सा यौवन-स्मित मधुप-सदृश निश्चिंत विहार।
भरी वासना-सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह,
प्रलय-जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा कराह।’
‘‘चिर-किशोर-वय, नित्यविलासी-सुरभित जिससे रहा दिगंत
आज तिरोहित हुआ कहां वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत ?
कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमलिंगन हुए विलीन,
मौन हुई है मूर्च्छित तानें और न सुन पड़ती अब बीन।
अब न कपोलों पर छाया-सी पड़ती मुख की सुरभित भाप,
भुज-भूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप।
कंकण क्वणित, रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार,
मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय को होता अभिसार।
सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक-अधीर,
सब में एक अचेतन गति थी, जिससे पिछड़ा रहे समीर।
वह अनंग-पीड़ा-अनुभव-सा अंग-भगियों का नर्तन,
मधुकर के मरंद-उत्सव-सा मदिर भाव से आवर्तन।
सुरा सुरभिमय बदन अरुण से नयन भरे आलस अनुराग,
कल कपोल था जहॉ बिछलता कल्पवृक्ष का पीत पराग।
विकल वासना के प्रतिनिधि से सब मुरझाये चले गये,
आह ! जले अपनी ज्वाला से सिर वे जल में गले, गये।’’
‘‘अरी अपेक्षा-भरी अमरते ! री अतृप्ति ! निर्बाध विलास !
द्विधा-रहित अपलक नयनों की भूख-भरी दर्शन की प्यास।
बिछुड़े सब तेरे आलिंगन, पुलक-स्पर्श का पता नहीं,
मधुमय चुंबन कातरतायें, आज न मुख को सता रहीं।
रत्न-सौध के वातायन- जिसमें आता मधु-मन्दर समीर,
टकराती होगी अब उनमें तिमिंगिलों की भीड़ अधीर।
देवकामिनी के नयनों से जहां नील नलिनों की सृष्टि-
होती थी, अब वहां हो रही प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि।
वे अम्लान-कुसुम-सुरभित-मणि-रचित मनोहर मालायें,
बनी श्रृंखला, जकड़ीं जिनमें विलासिनी सुर-बालायें।
देव-यजन के पशुयज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला,
जलनिधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला।’’
‘‘उनको देख कौन रोया यों अंतरिक्ष में बैठ अधीर !
व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय यह प्रालेय हलाहल नीर !
हाहाकार हुआ क्रंदनमय कठिन कुलिश होते थे चूर,
हुए दिगंत बधिर, भीषण रव बार-बार होता था क्रूर।
दिग्दाहों से घूम उठे, या जलधर उठे क्षितिज-तट के !
सघन गगन में भीमप्रकंपन, झंझा के चलते भटके।
अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई,
वरुण व्यस्त थे, घनी कालिमा स्तर-स्तर जमती पीन हुई।
पंचभूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के शकल-निपात
उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रहीं ज्यों खोया प्रात।
बार-बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष,
मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष।
उधर गरजतीं सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी,
चली आ रहीं फेन उगलती फन फैलाये व्यालों-सी।
धंसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वाला-मुखियों के निश्वास
और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास।
सबल तरंगाघातों से उस क्रुद्ध सिंधु के, विचलित-सी-
व्यस्त महाकच्छप-सी धरणी ऊभ-चूभ थी विकलित-सी।
बढ़ने लगा विलास-वेग-सा वह अतिभैरव जल-संधात,
तरल-तिमिर से प्रलय-पवन का होता आलिंगन, प्रतिघात।
बेला क्षण-क्षण निकट आ रही क्षितिज क्षीण, फिर लीन हुआ,
उदधि डुबाकर अखिल धारा को बस मर्यादा-हीन हुआ !
पंचभूत का यह तांडवमय नृत्य हो रहा था कब का।’’
‘‘एक नाव थी, और न उसमें डांड़े लगते, या पतवार,
तरल तरंगों में उठ-गिरकर बहती पगली बारंबार।
लगते प्रबल थपेड़े धुधले तट का था कुछ पता नहीं,
कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वहीं।
लहरें व्योम चूमती उठतीं, चपलायें असंख्य नचतीं,
गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदें निज संसृति रचतीं।
चपलायें उस जलधि-विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थीं,
ज्यों विराट बाड़व-ज्वालायें खंड-खंड हो रोती थीं।
जलनिधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते,
हुआ विलोड़ित गृह, तब प्राणी कौन! कहॉ! कब ! सुख पाते ?
घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध,
और चेतना थी विलखाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध।
उस विराट् आलोड़न में ग्रह, तारा बुद-बुद से लगते,
प्रखर प्रलय-पावस में जगमग, ज्योतिरिंगणों-से जलते।
प्रहर दिवस कितने बीते, अब इसको कौन बता सकता,
इनके सूचक उपकरणों को चिह्न न कोई पा सकता।
काला शासन-चक्र मृत्यु का कब तब चला, न स्मरण रहा,
महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा।
किंतु, उसी न ला टकराया इस उत्तरगिरि के शिर से,
देव-सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से।
आज अमरता का जीवित हूं मैं वह भीषण जर्जर दंभ,
आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम-पात्र मय सा विष्कंभ।’’
‘‘ओ जीवन की सरु-मीरीचिका, कायरता के अलस विषाद !
अरे पुरातन अमृत ! अगतिमय मोहमुग्ध जर्जर अवसाद !
मौन ! नाश ! विध्वंस ! अंधेरा ! शून्य बना जो प्रकट अभाव,
वहीं सत्य है, अरी अमरते ! तुझको ! यहां कहां अब ठांव।
मृत्यु, अरी चिर-निद्रे ! तेरा अंक हिमानी-सा शीतल,
तू अनंत में लहर बनाती काल-जलधि की-सी हलचल।
महानृत्य का विषम सम अरी अखिल स्पंदनों की तू माप,
तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप।
अंधकार के अट्टहास-सी मुखरित सतत चिरंतन सत्य,
छिपी सृष्टि के कण-कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य।
जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नीन धन-माला में,
सौदामिनी-संधि-सा सुन्दर क्षण भर रहा उजाला में।’’
पवन पी रहा था शब्दों को निर्जनता की उखड़ी सांस,
टकराती थी, दीन प्रतिध्वनि बनी हिम-शिलाओं के पास।
धू-धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य,
आकर्षण-विहीन विद्युत्कण बने भारवाही थे भृत्य।
मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती ती दृष्टि,
परमव्योम से भौतिक कण-सी घने कुहासों की थी वृष्टि।
वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल-संघात,
सौरचक्र में आवर्त्तन था प्रलय निशा का होता प्रात !
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i