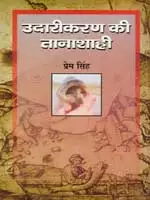|
अर्थशास्त्र >> उदारीकरण की तानाशाही उदारीकरण की तानाशाहीप्रेम सिंह
|
420 पाठक हैं |
|||||||
यह पुस्तक उदारीकरण-भूमंडलीकरण की परिघटना पर केन्द्रित है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
यह पुस्तक उदारीकरण-भूमंडलीकरण की परिघटना पर परिकेन्द्रित है। इसमें
उदारीकरण के नाम से प्रचारित नई आर्थिक नीतियों के देश की अर्थव्यवस्था और
राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। पुस्तक की
मुख्या स्थापना हैः वैश्विक आर्थिक संस्थाओं विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रीय
मुद्राकोष, विश्व व्यापार संगठन-और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के ‘डिक्टेट’ पर लादी जा रही आर्थिक गुलामी का नतीजा राजनैतिक गुलामी में निकलने लगा है।
इसके साथ यह भी दर्शाया गया है कि आर्थिक और राजनैतिक के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों पर भी उदारीकरण की तानाशाही चल रही है। इसके लिए अकेले राजनैतिक नैतृत्व को जिम्मेदार न मानकर, भूमंडलीकरण के समर्थक बुद्धिजीवियों और विदेशी धन लेकर एनजीओ चलाने वाले रोगों को भी जिम्मेदार माना गया है।
पुस्तक में भूमंडलीकरण को नवसाम्राज्यवाद का अग्रदूत मानते हुए साम्राज्यवादी सभ्यता के बरक्स वैकल्पिक सभ्यता के निर्माण की जरूरत पर बल दिया गया है।
पुस्तक में सारी बहस देश और दुनिया की वंचित आबादी से की गई है। इस रूप में यह सरोकारधर्मी और हस्तक्षेपकारी लेखन का सशक्त उदाहरण है।
भाषा की स्पष्टता और शैली की रोचकता पुस्तक को सामान्य पाठकों के लिए पठनीय बनाती है।
इसके साथ यह भी दर्शाया गया है कि आर्थिक और राजनैतिक के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों पर भी उदारीकरण की तानाशाही चल रही है। इसके लिए अकेले राजनैतिक नैतृत्व को जिम्मेदार न मानकर, भूमंडलीकरण के समर्थक बुद्धिजीवियों और विदेशी धन लेकर एनजीओ चलाने वाले रोगों को भी जिम्मेदार माना गया है।
पुस्तक में भूमंडलीकरण को नवसाम्राज्यवाद का अग्रदूत मानते हुए साम्राज्यवादी सभ्यता के बरक्स वैकल्पिक सभ्यता के निर्माण की जरूरत पर बल दिया गया है।
पुस्तक में सारी बहस देश और दुनिया की वंचित आबादी से की गई है। इस रूप में यह सरोकारधर्मी और हस्तक्षेपकारी लेखन का सशक्त उदाहरण है।
भाषा की स्पष्टता और शैली की रोचकता पुस्तक को सामान्य पाठकों के लिए पठनीय बनाती है।
प्राक्कथन
पिछली शताब्दी के अन्तिम दशक भारतीय राजनीति में खास मायने रखता है। इस
दौरान वे तीन परिघटनाएँ खुलकर सामने आ जाती हैं, जिनका बनाव उसके पिछले एक
दशक से बनता आ रहा था। ये हैं : सामप्रदायिकता, उदारीकरण-वैश्वीकरण और
प्रगतिशील राजनीति का गतिरोध। तीनों परिघटनाएँ अलग-अलग न होकर एक-दूसरे से
जुड़ी हुई हैं। कहा जा सकता है कि पहली दो परिघटनाओं ने एकजुट होकर देश की
प्रगतिशील राजनीति का तेज हर लिया है ये परिघटनाएँ केवल राजनीति तक सीमित
नहीं हैं। उनका हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अर्थात् समग्र
राष्ट्रीय जीवन पर गहरा और दूरगामी असर पड़ा है।
इन परिघटनाओं के स्रोत, स्वरूप, अन्तर्सम्बन्ध और प्रभावों को लेकर मैंने समय-समय पर विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं में लेख लिखे हैं। उनमें से पिछले करीब आठ सालों के दौरान लिखे गए कुछ लेख इस पुस्तक में संकलित हैं। इनमें मुख्यतः भूमंडलीकरण के प्रभाव का विश्लेषण हैं। इसके साथ बाकी लेखों से चुन कर दो और पुस्तकें तैयार की गई हैं : ‘कट्टरता जीतेगी या उदारता’ और ‘प्रगतिशील राजनीति का गतिरोध’। पहली में साम्प्रदायिकता की परिघटना से सम्बन्धित लेख हैं और दूसरी में प्रगतिशील राजनीति के गतिरोध से सम्बन्धित। तीनों पुस्तकें कुछ हद तक पिछले एक दशक की राजनीति और राष्ट्रीय जीवन पर उसके प्रभाव की तस्वीर पेश करती हैं।
लेख फुटकर रूप में लिखे गए हैं इसलिए उनमें दोहराव मिलेगा। सुधी पाठक इस गलती को इस तरह के लेखन की मजबूरी जान कर क्षमा करेंगे। मेरा इन लेखों के बारे में अकादमिक तटस्थता का दावा नहीं है। न ही अकादमिक उपलब्धि का। ये सभी लेख समाजवादी आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता के नाते लिखे गए हैं। मेरी जो भी थोड़ी बहुत प्रतिबद्धता है, उसके पीछे उन साथियों की अडिग निष्ठा और चरित्र का बल है, जो सम्प्रदायवादी और साम्राज्यवादी आक्रमण के खिलाफ समाज की वंचित आबादी के हक में निहत्थे और नंगे पाँव लोहा ले रहे हैं। उनका नाम देने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि वे नाम के लिए नहीं, एक बड़े उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
हिन्दू मजदूर सभा (एच.एम.एस.) के पूर्व महासचिव समाजवादी नेता और लेखक श्री बृजमोहन तूफान का व्यक्तित्व सम्पर्क में आनेवाले सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होता है। मुझे भी अपने कार्यों और लेखन के लिए उनसे निरन्तर प्रेरणा मिलती है। वरिष्ठ समाजवादी नेता और विचारक श्री सुरेन्द्र मोहन हर युवा कार्यकर्ता का लेखन चाव से पढ़ते और सराहते हैं। अगर लिखने में थोड़ा भी ‘गैप’ आता है, तो वे मुझे टोक देते हैं कि लिखना क्यों बन्द कर दिया है। विकल्प की राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर श्री किशन पटनायक का हवाला इन लेखों में जगह-जगह आया है समाजवादी आन्दोलन की दो निस्पृह विभूतियों श्री सच्चिदानन्द सिन्हा और श्री अशोक सेकसरिया बहुत से समाजवादी कार्यकर्ताओं की सक्रियता के साथ मेरा भी सम्बल हैं। इन विरल हस्तियों का साथ और स्नेह मिलना, जो मुझे भी मिला है, एक नियामत है।
मैंने पत्रकारी लेखन की शुरुआत ‘प्रतिपक्ष’ से की थी। उस समय साथी विनोद प्रसाद सिंह उसके सम्पादक थे। ‘नया संघर्ष’ में काम करते हुए वह सिलसिला आगे बढ़ा। साथी राजकिशोर, सुनील, अरविन्द मोहन, हरिमोहन, अरुण त्रिपाठी, सत्येन्द्र रंजन, शमसुल इस्लाम, डॉ. राकेश रफीक, प्रेमपाल शर्मा, डॉ. विक्रम सिंह, डॉ. पवन कुमार और डॉ. ए.के. अरुण के प्रोत्साहन और सुझावों की इन लेखों के पीछे महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रोफेसर रणधीर सिंह, प्रोफेसर नामवर सिंह, प्रोफेसर अनिल सदगोपाल, प्रोफेसर नित्यानन्द तिवारी, डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी और श्री भीष्म साहनी (दिवंगत) ने मुझे इस तरह के लेखन के लिए हमेशा प्रेरित किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू साथियों से मुझे लेखन समेत सभी कामों में भरपूर सहयोग मिलता है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक गतिविधियों में हिस्सेदारी और लेखन में व्यस्तता के चलते मेरी पत्नी कुमकुम यादव और बेटे सौरभ को बहुत सहना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि पुस्तक देखकर उन्हें खुशी होगी।
लेखों को पुस्तककार छपवाने की सलाह सबसे पहले प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने दी थी। उन्होंने ही राजकमल प्रकाशन के स्वामी श्री अशोक महेश्वरी से बात करने को कहा। उस समय मेरी तरफ से बात आई-गई हो गई। इधर अन्तरंग मित्र नानकचन्द ने रुचि लेकर अशोक जी से बात की। मुझे आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई, जब उन्होंने तत्काल पुस्तक छापना मंजूर कर लिया। मेरे मन में इन तीनों सज्जनों के लिए कृतज्ञता का भाव है। पुस्तक के ज्यादातर लेख जनसत्ता में छपे हैं। उसके अलावा हिन्दुस्तान और राष्ट्रीय सहारा में। इन अखबारों के सम्पादकों और सम्पादकीय पृष्ठ के प्रभारी साथी पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ। पुस्तक की सेटिंग करने के लिए साथी गोपाल और संजय शर्मा को भी उनकी अमूल्य मदद के लिए धन्यवाद देता हूँ।
इन परिघटनाओं के स्रोत, स्वरूप, अन्तर्सम्बन्ध और प्रभावों को लेकर मैंने समय-समय पर विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं में लेख लिखे हैं। उनमें से पिछले करीब आठ सालों के दौरान लिखे गए कुछ लेख इस पुस्तक में संकलित हैं। इनमें मुख्यतः भूमंडलीकरण के प्रभाव का विश्लेषण हैं। इसके साथ बाकी लेखों से चुन कर दो और पुस्तकें तैयार की गई हैं : ‘कट्टरता जीतेगी या उदारता’ और ‘प्रगतिशील राजनीति का गतिरोध’। पहली में साम्प्रदायिकता की परिघटना से सम्बन्धित लेख हैं और दूसरी में प्रगतिशील राजनीति के गतिरोध से सम्बन्धित। तीनों पुस्तकें कुछ हद तक पिछले एक दशक की राजनीति और राष्ट्रीय जीवन पर उसके प्रभाव की तस्वीर पेश करती हैं।
लेख फुटकर रूप में लिखे गए हैं इसलिए उनमें दोहराव मिलेगा। सुधी पाठक इस गलती को इस तरह के लेखन की मजबूरी जान कर क्षमा करेंगे। मेरा इन लेखों के बारे में अकादमिक तटस्थता का दावा नहीं है। न ही अकादमिक उपलब्धि का। ये सभी लेख समाजवादी आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता के नाते लिखे गए हैं। मेरी जो भी थोड़ी बहुत प्रतिबद्धता है, उसके पीछे उन साथियों की अडिग निष्ठा और चरित्र का बल है, जो सम्प्रदायवादी और साम्राज्यवादी आक्रमण के खिलाफ समाज की वंचित आबादी के हक में निहत्थे और नंगे पाँव लोहा ले रहे हैं। उनका नाम देने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि वे नाम के लिए नहीं, एक बड़े उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
हिन्दू मजदूर सभा (एच.एम.एस.) के पूर्व महासचिव समाजवादी नेता और लेखक श्री बृजमोहन तूफान का व्यक्तित्व सम्पर्क में आनेवाले सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होता है। मुझे भी अपने कार्यों और लेखन के लिए उनसे निरन्तर प्रेरणा मिलती है। वरिष्ठ समाजवादी नेता और विचारक श्री सुरेन्द्र मोहन हर युवा कार्यकर्ता का लेखन चाव से पढ़ते और सराहते हैं। अगर लिखने में थोड़ा भी ‘गैप’ आता है, तो वे मुझे टोक देते हैं कि लिखना क्यों बन्द कर दिया है। विकल्प की राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर श्री किशन पटनायक का हवाला इन लेखों में जगह-जगह आया है समाजवादी आन्दोलन की दो निस्पृह विभूतियों श्री सच्चिदानन्द सिन्हा और श्री अशोक सेकसरिया बहुत से समाजवादी कार्यकर्ताओं की सक्रियता के साथ मेरा भी सम्बल हैं। इन विरल हस्तियों का साथ और स्नेह मिलना, जो मुझे भी मिला है, एक नियामत है।
मैंने पत्रकारी लेखन की शुरुआत ‘प्रतिपक्ष’ से की थी। उस समय साथी विनोद प्रसाद सिंह उसके सम्पादक थे। ‘नया संघर्ष’ में काम करते हुए वह सिलसिला आगे बढ़ा। साथी राजकिशोर, सुनील, अरविन्द मोहन, हरिमोहन, अरुण त्रिपाठी, सत्येन्द्र रंजन, शमसुल इस्लाम, डॉ. राकेश रफीक, प्रेमपाल शर्मा, डॉ. विक्रम सिंह, डॉ. पवन कुमार और डॉ. ए.के. अरुण के प्रोत्साहन और सुझावों की इन लेखों के पीछे महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रोफेसर रणधीर सिंह, प्रोफेसर नामवर सिंह, प्रोफेसर अनिल सदगोपाल, प्रोफेसर नित्यानन्द तिवारी, डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी और श्री भीष्म साहनी (दिवंगत) ने मुझे इस तरह के लेखन के लिए हमेशा प्रेरित किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू साथियों से मुझे लेखन समेत सभी कामों में भरपूर सहयोग मिलता है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक गतिविधियों में हिस्सेदारी और लेखन में व्यस्तता के चलते मेरी पत्नी कुमकुम यादव और बेटे सौरभ को बहुत सहना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि पुस्तक देखकर उन्हें खुशी होगी।
लेखों को पुस्तककार छपवाने की सलाह सबसे पहले प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने दी थी। उन्होंने ही राजकमल प्रकाशन के स्वामी श्री अशोक महेश्वरी से बात करने को कहा। उस समय मेरी तरफ से बात आई-गई हो गई। इधर अन्तरंग मित्र नानकचन्द ने रुचि लेकर अशोक जी से बात की। मुझे आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई, जब उन्होंने तत्काल पुस्तक छापना मंजूर कर लिया। मेरे मन में इन तीनों सज्जनों के लिए कृतज्ञता का भाव है। पुस्तक के ज्यादातर लेख जनसत्ता में छपे हैं। उसके अलावा हिन्दुस्तान और राष्ट्रीय सहारा में। इन अखबारों के सम्पादकों और सम्पादकीय पृष्ठ के प्रभारी साथी पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ। पुस्तक की सेटिंग करने के लिए साथी गोपाल और संजय शर्मा को भी उनकी अमूल्य मदद के लिए धन्यवाद देता हूँ।
प्रेम
सिंह
उदारीकरण और तानाशाही
सिएटल में आयोजित वार्ता का दौर भले ही फेल हो गया हो और प्रधानमन्त्री को
उस पर अफसोस हो, भारत वैश्वीकरण-उदारीकरण की चाल पर कायम है। देश के
राष्ट्रपति को सौंपे गए करोड़ों लोगों के हस्ताक्षरों देश भर में फैले
बीमा कर्मचारियों के प्रतिरोधात्मक आन्दोलन और कई राजनैतिक पार्टियों के
नेताओं के लोकसभा से बहिर्गमन के बावजूद बीमा विनिमयन एवं विकास प्राधिकरण
विधेयक पास हो गया। कुछ देर तक समर्थन के बदले बोफोर्स चार्जशीट से
स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम हटाने की जिद करने के बाद कांग्रेस ने अपने
कुछ संशोधन मनवाकर अन्ततः रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा दी। आखिर अपने
बच्चे को माँ कब तक दूध न पिलाती ! बहरहाल, लम्बे समय से लटके बीमा विधेयक
को पास होना ही था, सो वह हो गया विरोध करनेवाले मुख्यधारा राजनीति के
नेताओं ने भी अपने राज में उसे पास कराने की पूरी कोशिश की ही थी। संसद के
भीतर और बाहर के विरोध में जब अपेक्षित दम था ही नहीं, तो उसका पास होना
तय था।
यहाँ भारत में उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह का स्मरण करें। सबसे पहले वे नरसिम्हा राव के जमूरे बनकर राजनैतिक मंच पर उतरे थे, फिर सीमाराम केसरी ने उन्हें उतारा और अब वे सोनिया गांधी के बगलगीर हैं। ये मनमोहन सिंह ही थे, जिन्होंने भारतीय सरकार की वैधता को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सन्दर्भ में आँकने की कसौटी रखी थी। देवगौड़ा जब प्रधानमन्त्री थे, तो उन्होंने कहा सरकार की नीतियों-वर्तमान दौर में नीतियों से आशय केवल नई आर्थिक नीति रह गया है, इसमें और संकुचन आ जाता है, जब आर्थिक नीति से आशय विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की आर्थिक नीति होता है-के चलते बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में अनिश्चय का भाव बना हुआ है। यानी सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ निश्शंक होकर अपना व्यापार चला सकें। मनमोहन सिंह की मान्यता के आर्थिक पहलू की बात न करके, राजनैतिक पहल की बात करें, जो काफी उद्घाटक है। अब न केवल राजनीति की प्राथमिकता की जगह अर्थनीति ले रही है, भारत सरकार की वैधता का प्रतिमान भी उलट रहा है।
सरकार की वैधता की परख अब इस देश और समाज के सन्दर्भ में न होकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सन्दर्भ में होगी ! विश्व-व्यवस्था का स्वप्नद्रष्टा भारत सरकार के स्थानीय वैधता के प्रतिमान से चिपका नहीं रह सकता ! दरअसल, मनमोहन सिंह का प्रतिमान उनकी विचारधारा की पूर्ण संगति में है। अगर यह मनमोहन सिंह का अकेला और निजी प्रतिमान होता, तो उतनी चिन्ता की बात नहीं होती। चिन्ता तब होती है जब एक के बाद एक आनेवाला प्रधानमन्त्री और वित्तमन्त्री उसी प्रतिमान के तहत सरकार की वैधता सिद्ध करने की तत्परता दिखाता है। इस प्रतिमान के विरोध की जहाँ सम्भावनाएँ हैं, वहाँ से भी मजबूत प्रतिरोध खड़ा नहीं हो पाता। मार्क्सवादी सहयोग-विरोध की द्वन्द्वात्मकता में फँसकर रह जाते हैं और नई चुनावी राजनीति के पुरोधा पिछड़े और दलित नेताचुनावी जीत की लिप्सा में यह सोच ही नहीं पाते कि दलित और पिछड़े भारत के जाग्रत हो जाने पर, भारत सरकार की वैधता का प्रतिमान क्या होगा और उसे कौन तय करेगा। वे अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय किस्म के मसलों में पड़कर अपनी ‘लड़ाई’ को धीमा नहीं करना चाहते। इससे क्या कि वह केवल नेतागिरी जमाने की लड़ाई है !
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के तेज के सामने भाजपा के राष्ट्र प्रेम की चमक भी मलिन पड़ जाती है। बस इतना ही सन्तोष बचा रहता है कि कैसी भी हो, हम सरकार में हैं। वैचारिक रूप से भाजपा की स्थिति दलित और पिछड़े नेताओं से भी पतली ठहरती है, भले ही थिंकटैंक’ और सवर्णों का बल उसके पास हो। दलित और पिछड़े नेताओं की सोच में आनेवाला भारत भाजपा की सोच में आनेवाले भारत से बड़ा है। बहरहाल, ध्यान देने की बात यह है कि अर्थनीति को गिरवी रखने का परिणाम राजनीति को गिरवी रखने में निकलने लगा है, जिसकी चिन्ता किसी भी राष्ट्रीय नेता या पार्टी को नहीं व्यापती। दरअसल यह मुख्यधारा राजनीति की चाल की संगति में ही है। अलबत्ता साम्राज्यवाद ने जरूर अपनी चाल उलट दी है : पहले उसने राजनीति पर कब्जे के बाद अर्थनीति पर कब्जा किया था, अब अर्थनीति पर कब्जा करके राजनीति पर कब्जा जमाने की योजना चल रही है। इसका प्रमुख कारण तो यही है कि यह रिमोट कन्ट्रोल का जमाना है। लेकिन साथ ही विश्वविजेताओं को लगता होगा कि 1857 और 1942 जैसे जनान्दोलनों को सीधे झेलने से बचा जाए। भूखे लोग लड़ते हैं मार्क्स का यह कथन उन्हें अभी भी डराता होगा-भूख केवल पेट की नहीं, आत्म और राष्ट्रीय सम्मान की भी। लिहाजा नवउपनिवेश में ही एक ऐसा एलीट तबका स्थापित कर दिया जाए, जो कार्यवादी को अंजाम दे और विरोध को खारिज करे, न हो तो उसका दमन करे। इस एलीट तबके में शामिल भारतीय अंग्रेजी मीडिया की भूमिका पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसका अनुकरण कुछ भाषायी पत्रकार भी अपने नेता या पार्टी के दवाब में करते हैं।
बीमा विधेयक पास होने पर राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषा भी मानो पास हो गई है। सभी जानते हैं कि ज्यादातर अंग्रेजी मीडिया उदारीकरण का पक्षधर है और पक्षधरता के उसके तर्क अक्सर वस्तुनिष्ठता से रहित और एकांगी होते हैं। नई अर्थनीति विषयक उसका चिन्तन और समर्थन गरीब भारत की चिन्ता से प्रायः मुक्त होता है। और इस सच्चाई से कौन इनकार करेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में गरीब भारत की व्याप्ति अमीर भारत के मुकाबले हजारों हजार गुना ज्यादा है और उसकी समस्याएँ भी। इधर सरकार गिरने और चुनाव होकर फिर बनने की-अंग्रेजी मीडिया की नजर में ‘बेजा’ प्रक्रिया के चलते उदारीकरण की रफ्तार कुछ धीमी हो चली थी। चुनावों के दौरान सभी पार्टियों के नेताओं को वोट की मजबूरी में गरीब भारत के बीच भी जाना पड़ा था और उसके कल्याण की भी कुछ बातें कहनी पड़ी थीं। अमीर भारत के संरक्षण में जुटे संरक्षणवाद विरोधी अंग्रेजी मीडिया को यह सब बड़ा नागवार गुजरा था। लिहाजा, उसने बीमा विधेयक के मामले में आक्रामक और अन्धा रुख अपनाया, ताकि उदारीकरण की रफ्तार को फिर से तेजी प्रदान की जा सके। उसने मनमोहन सिंह की लाइन पर बीमा विधेयक के राष्ट्रहित का वास्ता जोड़ते हुए उसे पास करनेवालों को राष्ट्रभक्ति की परीक्षा में पास और विरोध करनेवालों को फेल घोषित कर दिया है। शुरू में कांग्रेस की नानुच को उसने सीधे राष्ट्रविरोधी करार दिया।
जैसे ही कांग्रेस ने विधेयक के पक्ष में मत बनाया, वैसे ही अंग्रेजी मीडिया की नजर में कांग्रेस राष्ट्र की हित साधक पार्टी हो गई और सोनिया गांधी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय नेता। अंग्रेजी मीडिया ने कांग्रेस के भीतर विधेयक के विरोध में उठनेवाले स्वरों को दबा कर पार्टी को विधेयक के पक्ष में लामबन्द करने के लिए सोनिया गांधी के नेतृत्व की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। उसे विश्वास है कि सोनिया गांधी इसी तरह पार्टीगत हितों, से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर का आचरण करती रहें, तो वह उसे राष्ट्रीय नेता बना देगा। सोनिया गांधी ने भी समझ लिया होगा कि नित-नूतन चाहनेवाला अमीर भारत, जब भाजपा की राष्ट्रभक्ति से ऊब जाएगा, तो अंग्रेजी मीडिया राष्ट्र (भक्ति) की बागडोर उनके हाथ में थमा सकता है।
अंग्रेजी मीडिया ने बात साफ कर दी है : जो उदारीकरण के पक्ष में है वह राष्ट्रहितैषी है और जो विरोध में है वह राष्ट्रविरोधी। राष्ट्रभक्ति के अपने इस मानक के निर्धारण में अंग्रेजी मीडिया किसी बहस की गुंजाइश छोड़ने को तैयार नहीं है। हालाँकि इसके बावजूद वह लोकतन्त्र विरोधी होने का आक्षेप बरदाश्त नहीं कर सकता ! लोकतन्त्र (अभिजात-तन्त्र पढ़ा जाए) की उसकी अपनी परिभाषा है, जिसे वह सभी पर लादना चाहता है और विरोध करनेवालों को पार्टीजन कह कर खारिज कर देता है। दूसरे शब्दों में, जो लोकतन्त्र बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों से वैधता हासिल करने को तैयार नहीं है, वह अंग्रेजी मीडिया की परिभाषा में लोकतन्त्र नहीं है। उसके लिए लोकतन्त्र वही है जो उदारीकरण की तानाशाही स्वीकार करके चले। प्रेस को लोकतन्त्र का चौथा खम्भा कहा जाता है। जाहिर है, अंग्रेजी मीडिया अपने को ‘अभिजात तन्त्र’ का चौथा खम्भा मानता है।
इस अभिजात-तन्त्र में हड़ताल या प्रतिरोध के अन्य तरीके ब्लैकमेलिंग करार दिए जाते हैं। पिछले दिनों ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल को इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान सम्पादक शेखर गुप्ता ने एक टीवी चैनल पर खुलेआम ब्लैकमेलिंग कहा था। जो न सुन पाए हों, उन्हें पढ़ाने के लिए अखबार के सम्पादकीय में भी यह मान्यता दोहरा दी गई थी। बीमा क्षेत्र के कर्मचारी लम्बे समय से आन्दोलन की राह पर हैं। अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी भी अपनी माँगों को लेकर समय-समय पर प्रदर्शन और हड़ताल आदि करते हैं। किसान और अन्य उत्पादक कामों में जुटे समूह भी बीच-बीच में आन्दोलित होते रहते हैं। जाहिर है, अंग्रेजी मीडिया की नजर में उन सभी का आन्दोलन राष्ट्रविरोधी ठहरता है।
इक्कीसवीं सदी में जाने की बड़ी भारी चर्चा चल रही है। ध्यान देना होगा कि अंग्रेजी मीडिया ने इक्कीसवीं सदी के लिए राष्ट्रहित और राष्ट्रभक्ति का अपना एजेंडा निर्धारित कर दिया है, जिस पर वह लगातार बल बनाए रहेगा। मनमोहन सिंह ने भारतीय सरकार की वैधता को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सन्दर्भ में आँकने की जो कसौटी रखी थी, उसे कायम रखने की अंग्रेजी मीडिया भरपूर कोशिश करेगा। पिछले चुनावों में सुन रहे थे कि सोनिया गांधी जीतने पर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमन्त्री बना सकती हैं। कांग्रेस तो हारी ही, खुद मनमोहन सिंह भी चुनाव हार गए। लेकिन वे खुश हो सकते हैं कि उनके राजनैतिक बच्चे उनके नीतिगत बच्चे का पालन-पोषण पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं और आगे भी करने का मजबूत इरादा रखते हैं।
अभी तो खैर भाजपा सत्ता में है, जो साम्प्रदायिकता के साथ-साथ उदारीकरण भी वैसी ही रफ्तार से चला रही है। समस्या और जटिल हो जाती है, भाजपा को सत्ता से बाहर रखने की बिना पर धर्मनिरपेक्षतावादी पार्टियों को जब सत्ता मिलती है, तो वे भी उसका ‘उपयोग’ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का हुक्म बजाने में ही करती हैं। उनमें भी मनमोहन सिंह के प्रतिमान पर खरा उतरने की बेताबी होती है। गरीब भारत विरोधी उदारीकरण के विरुद्ध सच्चे और सार्थक विचारों/आन्दोलनों से की उपेक्षा यह जताकर की जाती है कि अगर सरकार अस्थिर की जाएगी तो भाजपा आ जाएगी, जो साम्प्रदायिकता के साथ उदारीकरण भी जारी रखेगी। वैसे में उदारीकरण का विरोध करनेवाले गैर राजनैतिक समूहों और बौद्धिकों को अपने से कुछ नई युक्तियाँ सोचनी होंगी, ताकि सारा उद्यम और ऊर्जा बेकार न चले जाएँ और इक्कीसवीं सदी में अन्ततः अवसाद और हताशा का बोध न घेर ले इस समस्यात्मक विषय पर गम्भीर विचार विमर्श चलाने की जरूरत है, जिसके नतीजे में साम्प्रदायिकता और उदारीकरण को एक साथ निष्क्रिय करनेवाली विचारधारा और कार्यक्रम पाया जा सके। सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की बैठक पर हुए प्रतिरोध का अध्ययन इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि उससे विकासशील देशों के उदारीकरण विरोधी संगठनों के लिए क्या सार्थक सूत्र हासिल किए जा सकते हैं।
यहाँ भारत में उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह का स्मरण करें। सबसे पहले वे नरसिम्हा राव के जमूरे बनकर राजनैतिक मंच पर उतरे थे, फिर सीमाराम केसरी ने उन्हें उतारा और अब वे सोनिया गांधी के बगलगीर हैं। ये मनमोहन सिंह ही थे, जिन्होंने भारतीय सरकार की वैधता को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सन्दर्भ में आँकने की कसौटी रखी थी। देवगौड़ा जब प्रधानमन्त्री थे, तो उन्होंने कहा सरकार की नीतियों-वर्तमान दौर में नीतियों से आशय केवल नई आर्थिक नीति रह गया है, इसमें और संकुचन आ जाता है, जब आर्थिक नीति से आशय विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की आर्थिक नीति होता है-के चलते बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में अनिश्चय का भाव बना हुआ है। यानी सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ निश्शंक होकर अपना व्यापार चला सकें। मनमोहन सिंह की मान्यता के आर्थिक पहलू की बात न करके, राजनैतिक पहल की बात करें, जो काफी उद्घाटक है। अब न केवल राजनीति की प्राथमिकता की जगह अर्थनीति ले रही है, भारत सरकार की वैधता का प्रतिमान भी उलट रहा है।
सरकार की वैधता की परख अब इस देश और समाज के सन्दर्भ में न होकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सन्दर्भ में होगी ! विश्व-व्यवस्था का स्वप्नद्रष्टा भारत सरकार के स्थानीय वैधता के प्रतिमान से चिपका नहीं रह सकता ! दरअसल, मनमोहन सिंह का प्रतिमान उनकी विचारधारा की पूर्ण संगति में है। अगर यह मनमोहन सिंह का अकेला और निजी प्रतिमान होता, तो उतनी चिन्ता की बात नहीं होती। चिन्ता तब होती है जब एक के बाद एक आनेवाला प्रधानमन्त्री और वित्तमन्त्री उसी प्रतिमान के तहत सरकार की वैधता सिद्ध करने की तत्परता दिखाता है। इस प्रतिमान के विरोध की जहाँ सम्भावनाएँ हैं, वहाँ से भी मजबूत प्रतिरोध खड़ा नहीं हो पाता। मार्क्सवादी सहयोग-विरोध की द्वन्द्वात्मकता में फँसकर रह जाते हैं और नई चुनावी राजनीति के पुरोधा पिछड़े और दलित नेताचुनावी जीत की लिप्सा में यह सोच ही नहीं पाते कि दलित और पिछड़े भारत के जाग्रत हो जाने पर, भारत सरकार की वैधता का प्रतिमान क्या होगा और उसे कौन तय करेगा। वे अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय किस्म के मसलों में पड़कर अपनी ‘लड़ाई’ को धीमा नहीं करना चाहते। इससे क्या कि वह केवल नेतागिरी जमाने की लड़ाई है !
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के तेज के सामने भाजपा के राष्ट्र प्रेम की चमक भी मलिन पड़ जाती है। बस इतना ही सन्तोष बचा रहता है कि कैसी भी हो, हम सरकार में हैं। वैचारिक रूप से भाजपा की स्थिति दलित और पिछड़े नेताओं से भी पतली ठहरती है, भले ही थिंकटैंक’ और सवर्णों का बल उसके पास हो। दलित और पिछड़े नेताओं की सोच में आनेवाला भारत भाजपा की सोच में आनेवाले भारत से बड़ा है। बहरहाल, ध्यान देने की बात यह है कि अर्थनीति को गिरवी रखने का परिणाम राजनीति को गिरवी रखने में निकलने लगा है, जिसकी चिन्ता किसी भी राष्ट्रीय नेता या पार्टी को नहीं व्यापती। दरअसल यह मुख्यधारा राजनीति की चाल की संगति में ही है। अलबत्ता साम्राज्यवाद ने जरूर अपनी चाल उलट दी है : पहले उसने राजनीति पर कब्जे के बाद अर्थनीति पर कब्जा किया था, अब अर्थनीति पर कब्जा करके राजनीति पर कब्जा जमाने की योजना चल रही है। इसका प्रमुख कारण तो यही है कि यह रिमोट कन्ट्रोल का जमाना है। लेकिन साथ ही विश्वविजेताओं को लगता होगा कि 1857 और 1942 जैसे जनान्दोलनों को सीधे झेलने से बचा जाए। भूखे लोग लड़ते हैं मार्क्स का यह कथन उन्हें अभी भी डराता होगा-भूख केवल पेट की नहीं, आत्म और राष्ट्रीय सम्मान की भी। लिहाजा नवउपनिवेश में ही एक ऐसा एलीट तबका स्थापित कर दिया जाए, जो कार्यवादी को अंजाम दे और विरोध को खारिज करे, न हो तो उसका दमन करे। इस एलीट तबके में शामिल भारतीय अंग्रेजी मीडिया की भूमिका पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसका अनुकरण कुछ भाषायी पत्रकार भी अपने नेता या पार्टी के दवाब में करते हैं।
बीमा विधेयक पास होने पर राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषा भी मानो पास हो गई है। सभी जानते हैं कि ज्यादातर अंग्रेजी मीडिया उदारीकरण का पक्षधर है और पक्षधरता के उसके तर्क अक्सर वस्तुनिष्ठता से रहित और एकांगी होते हैं। नई अर्थनीति विषयक उसका चिन्तन और समर्थन गरीब भारत की चिन्ता से प्रायः मुक्त होता है। और इस सच्चाई से कौन इनकार करेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में गरीब भारत की व्याप्ति अमीर भारत के मुकाबले हजारों हजार गुना ज्यादा है और उसकी समस्याएँ भी। इधर सरकार गिरने और चुनाव होकर फिर बनने की-अंग्रेजी मीडिया की नजर में ‘बेजा’ प्रक्रिया के चलते उदारीकरण की रफ्तार कुछ धीमी हो चली थी। चुनावों के दौरान सभी पार्टियों के नेताओं को वोट की मजबूरी में गरीब भारत के बीच भी जाना पड़ा था और उसके कल्याण की भी कुछ बातें कहनी पड़ी थीं। अमीर भारत के संरक्षण में जुटे संरक्षणवाद विरोधी अंग्रेजी मीडिया को यह सब बड़ा नागवार गुजरा था। लिहाजा, उसने बीमा विधेयक के मामले में आक्रामक और अन्धा रुख अपनाया, ताकि उदारीकरण की रफ्तार को फिर से तेजी प्रदान की जा सके। उसने मनमोहन सिंह की लाइन पर बीमा विधेयक के राष्ट्रहित का वास्ता जोड़ते हुए उसे पास करनेवालों को राष्ट्रभक्ति की परीक्षा में पास और विरोध करनेवालों को फेल घोषित कर दिया है। शुरू में कांग्रेस की नानुच को उसने सीधे राष्ट्रविरोधी करार दिया।
जैसे ही कांग्रेस ने विधेयक के पक्ष में मत बनाया, वैसे ही अंग्रेजी मीडिया की नजर में कांग्रेस राष्ट्र की हित साधक पार्टी हो गई और सोनिया गांधी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय नेता। अंग्रेजी मीडिया ने कांग्रेस के भीतर विधेयक के विरोध में उठनेवाले स्वरों को दबा कर पार्टी को विधेयक के पक्ष में लामबन्द करने के लिए सोनिया गांधी के नेतृत्व की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। उसे विश्वास है कि सोनिया गांधी इसी तरह पार्टीगत हितों, से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर का आचरण करती रहें, तो वह उसे राष्ट्रीय नेता बना देगा। सोनिया गांधी ने भी समझ लिया होगा कि नित-नूतन चाहनेवाला अमीर भारत, जब भाजपा की राष्ट्रभक्ति से ऊब जाएगा, तो अंग्रेजी मीडिया राष्ट्र (भक्ति) की बागडोर उनके हाथ में थमा सकता है।
अंग्रेजी मीडिया ने बात साफ कर दी है : जो उदारीकरण के पक्ष में है वह राष्ट्रहितैषी है और जो विरोध में है वह राष्ट्रविरोधी। राष्ट्रभक्ति के अपने इस मानक के निर्धारण में अंग्रेजी मीडिया किसी बहस की गुंजाइश छोड़ने को तैयार नहीं है। हालाँकि इसके बावजूद वह लोकतन्त्र विरोधी होने का आक्षेप बरदाश्त नहीं कर सकता ! लोकतन्त्र (अभिजात-तन्त्र पढ़ा जाए) की उसकी अपनी परिभाषा है, जिसे वह सभी पर लादना चाहता है और विरोध करनेवालों को पार्टीजन कह कर खारिज कर देता है। दूसरे शब्दों में, जो लोकतन्त्र बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों से वैधता हासिल करने को तैयार नहीं है, वह अंग्रेजी मीडिया की परिभाषा में लोकतन्त्र नहीं है। उसके लिए लोकतन्त्र वही है जो उदारीकरण की तानाशाही स्वीकार करके चले। प्रेस को लोकतन्त्र का चौथा खम्भा कहा जाता है। जाहिर है, अंग्रेजी मीडिया अपने को ‘अभिजात तन्त्र’ का चौथा खम्भा मानता है।
इस अभिजात-तन्त्र में हड़ताल या प्रतिरोध के अन्य तरीके ब्लैकमेलिंग करार दिए जाते हैं। पिछले दिनों ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल को इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान सम्पादक शेखर गुप्ता ने एक टीवी चैनल पर खुलेआम ब्लैकमेलिंग कहा था। जो न सुन पाए हों, उन्हें पढ़ाने के लिए अखबार के सम्पादकीय में भी यह मान्यता दोहरा दी गई थी। बीमा क्षेत्र के कर्मचारी लम्बे समय से आन्दोलन की राह पर हैं। अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी भी अपनी माँगों को लेकर समय-समय पर प्रदर्शन और हड़ताल आदि करते हैं। किसान और अन्य उत्पादक कामों में जुटे समूह भी बीच-बीच में आन्दोलित होते रहते हैं। जाहिर है, अंग्रेजी मीडिया की नजर में उन सभी का आन्दोलन राष्ट्रविरोधी ठहरता है।
इक्कीसवीं सदी में जाने की बड़ी भारी चर्चा चल रही है। ध्यान देना होगा कि अंग्रेजी मीडिया ने इक्कीसवीं सदी के लिए राष्ट्रहित और राष्ट्रभक्ति का अपना एजेंडा निर्धारित कर दिया है, जिस पर वह लगातार बल बनाए रहेगा। मनमोहन सिंह ने भारतीय सरकार की वैधता को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सन्दर्भ में आँकने की जो कसौटी रखी थी, उसे कायम रखने की अंग्रेजी मीडिया भरपूर कोशिश करेगा। पिछले चुनावों में सुन रहे थे कि सोनिया गांधी जीतने पर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमन्त्री बना सकती हैं। कांग्रेस तो हारी ही, खुद मनमोहन सिंह भी चुनाव हार गए। लेकिन वे खुश हो सकते हैं कि उनके राजनैतिक बच्चे उनके नीतिगत बच्चे का पालन-पोषण पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं और आगे भी करने का मजबूत इरादा रखते हैं।
अभी तो खैर भाजपा सत्ता में है, जो साम्प्रदायिकता के साथ-साथ उदारीकरण भी वैसी ही रफ्तार से चला रही है। समस्या और जटिल हो जाती है, भाजपा को सत्ता से बाहर रखने की बिना पर धर्मनिरपेक्षतावादी पार्टियों को जब सत्ता मिलती है, तो वे भी उसका ‘उपयोग’ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का हुक्म बजाने में ही करती हैं। उनमें भी मनमोहन सिंह के प्रतिमान पर खरा उतरने की बेताबी होती है। गरीब भारत विरोधी उदारीकरण के विरुद्ध सच्चे और सार्थक विचारों/आन्दोलनों से की उपेक्षा यह जताकर की जाती है कि अगर सरकार अस्थिर की जाएगी तो भाजपा आ जाएगी, जो साम्प्रदायिकता के साथ उदारीकरण भी जारी रखेगी। वैसे में उदारीकरण का विरोध करनेवाले गैर राजनैतिक समूहों और बौद्धिकों को अपने से कुछ नई युक्तियाँ सोचनी होंगी, ताकि सारा उद्यम और ऊर्जा बेकार न चले जाएँ और इक्कीसवीं सदी में अन्ततः अवसाद और हताशा का बोध न घेर ले इस समस्यात्मक विषय पर गम्भीर विचार विमर्श चलाने की जरूरत है, जिसके नतीजे में साम्प्रदायिकता और उदारीकरण को एक साथ निष्क्रिय करनेवाली विचारधारा और कार्यक्रम पाया जा सके। सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की बैठक पर हुए प्रतिरोध का अध्ययन इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि उससे विकासशील देशों के उदारीकरण विरोधी संगठनों के लिए क्या सार्थक सूत्र हासिल किए जा सकते हैं।
अश्लीलता का विस्तार
अश्लीलता और नैतिकता पर बहस पुरानी है। आदिम से सांस्कृतिक सामाजिक होने
की प्रक्रिया में ही अश्लीलता और नैतिकता के सवाल पर विचार होना शुरू हो
गया होगा। ऐसा माना जाता है कि अश्लील शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त
‘अश्रीर’ शब्द जिसका सायण ने पहले स्थान पर अश्लील और
दूसरे
स्थान पर श्रीहीन गुण-विहीन और कुत्सित अर्थ किया है, का ही रूपान्तर है।
भारत और पश्चिम के काव्यशास्त्रियों ने अश्लीलता का विस्तृत विवेचन किया
है। काव्यशास्त्रियों ने अश्लीलता की सौन्दर्यबोध के सन्दर्भ में व्याख्या
करते हुए उसे एक काव्य दोष माना है, जबकि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों
समाजशास्त्रियों, न्यायविदों आदि ने अश्लीलता की प्रकृति और परिभाषा के
विषय में व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता के सन्दर्भ में विचार किया है।
इसके साथ ही आधुनिक राज्य व्यवस्थाओं में अश्लीलता को अपराध मानकर उसकी
रोकथाम के लिए कानून बनाए हैं। इन कानूनों के औचित्य अनौचित्य पर लगातार
बहस चलती रहती है।
केट मिलेट और अन्य कई आलोचकों ने अश्लीलता का स्त्रीवादी विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया है। इस सारे विवेचन की सीमा यह है कि वह अधिकांशतः लिखित साहित्य के सन्दर्भ में हुआ है। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के उच्च-प्रौद्यौगिकी युग में प्रचलित फीचर फिल्मों, गैर फीचर फिल्मों, टेलिविजन, टेबल एवं इंटरनेट प्रसारणों में अश्लीलता का सवाल नए सिरे से विवेचन की चुनौती उपस्थित करता है। जहाँ तक अवैध रूप से प्रसारित नग्न यौनाचार (पोर्नोग्राफी) का सवाल है, उसे सीधे कानूनन प्रतिबन्धित किया जा सकता है। वैसे प्रसारणों पर प्रतिबन्ध होता भी है। इनका निर्माण और प्रदर्शन समाज और कानून की निगाह से छिपकर किया जाता है। बच्चे और किशोर, जिनके ऊपर अश्लीलता के दुष्प्रभाव की सर्वाधिक चिन्ता की जाती है उनसे कुछ हद तक बचे रहे सकते हैं। लेकिन बाकी बचा जो कानूनसम्मत प्रसारण है, उसमें भी अश्लीलता का सवाल सुलझा हुआ नहीं है और अक्सर बहस का विषय बनता रहता है।
इधर पिछले कुछ वर्षों से फिल्मी तथा गैर फिल्मी नाच गानों के अलबमों और कुछ विज्ञापनों में स्त्री के शरीर की झटकेदार-मसालेदार नुमाइश भारतीय समाज के सन्दर्भ में अभूतपूर्व कही जाएगी। नग्न यौनाचार की हदों को छूता मसाला रमणियों का देह-प्रदर्शन कैसे भी कलात्मक और नैतिक मानदंडों से स्खलित, महज कामोत्तेजक होता है। सम्भवतः सौन्दर्य पहली बार इतना श्रीहीन और कुत्सित हुआ है। हालाँकि, साहित्य, स्थापत्य और चित्रकलाओं में बहुत पहले से स्त्री-शरीर और काम-चेष्टाओं का चित्रण पढ़ने-देखने को मिलता है, लेकिन नई लहर की विशिष्टता यह है उसमें शुरू से आखिर तक बाजारूपन तारी है। बाजारूपन के सभी मायनों के साथ, इस मायने में भी कि वह सबके ‘कंजप्शन’ के लिए होता है। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की क्रान्ति के चलते इसकी पहुँच समाज के हर तबके और हर उम्र के दर्शकों के लिए एक साथ है। इंटरनेट के जरिए कानूनन प्रतिबन्धित नग्न यौनाचार भी अब सर्वसुलभ है। यानी वैश्वीकरण केवल व्यापार का नहीं, देह-व्यापार का भी हो रहा है। भारत समेत प्रायः सभी आधुनिकता पूर्व समाजों में स्त्री-देह के प्रति भोगवादी बुद्धि की प्रधानता रही है। आधुनिक काल में उसके साथ मुनाफाखोर बुद्धि जुड़ गई है। पूँजीवादी व्यवस्था में हखियारों और नशीली वस्तुओं के साथ स्त्री देह भी मुनाफाखोरी का जबरदस्त जरिया है।
शर्त यही है कि प्रदर्शन जितना अश्लील होगा, मुनाफा भी उतना ही ज्यादा होगा। नग्न यौनाचार अगर अकूत मुनाफे का सौदा है तो इसीलिए कि उसमें अश्लीलता की कोई सीमा स्वीकार नहीं की जाती। नीली फिल्मों के अथाह समुद्र का विश्लेषण इस लेख का विषय नहीं है। यहाँ उस समुद्र के किनारों पर दिखाई देनेवाली अश्लीलता पर चर्चा की गई है। जाहिर है, जो किनारे पर है, उसका रिश्ता गहराइयों से है। किनारे पर खुला खेल खेलनेवाली स्त्रियाँ और उनके उद्यम को भारतीय समाज में आए खुलेपन का गुण बतानेवाले कतिपय फिल्मों के समाजशास्त्रियों को इस पर कड़ी आपत्ति होगी कि देह-प्रदर्शन को देह व्यापार (जिस्म फरोशी या वेश्यावृत्ति) से जोड़ा जाए। इस पर थोड़ा विचार कुछ देर बाद किया गया है कि आधुनिक देह-प्रदर्शन आधुनिक देह-व्यापार का ही एक रूप है और परम्परागत देह व्यापार से कहीं ज्यादा अनैतिक कर्म है।
स्त्री-देह की कानूनन प्रतिबन्धित और कानून सम्मत प्रदर्शन की परिघटना का स्रोत पूँजावादी अमरीका और पश्चिमी यूरोप के देश हैं। लैटिन अमरीका, अफ्रीका पूर्वी एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में तो इस परिघटना ने काफी पहले पहुँच बना ली थी, वैश्वीकरण की मुहिम के साथ भारत सहित बाकी के देशों में भी उसका तेजी से प्रवेश हुआ है। बहुलतावाद की बात करनेवाली उत्तर आधुनिक विचारधारा, उच्च पूँजीवाद जिसका व्यवस्थागत आधार है, में सभी समाजों और सभी उम्र के दर्शकों के लिए सुलभ एकरूप खुलापन परोसा जा रहा है। शायद आगे दस वर्ष भी न लगें जब भारत में भी फिल्मों और गैर फिल्मी नाच गानों के अलबमों में वैसी ही मैथुन मुद्राओं का प्रदर्शन होने लगे, जैसा हॉलीवुड, विकसित विश्व की अनेकानेक नाचमंडलियों और फैशन परेडों की प्रस्तुतियों में होता है। आगे चलकर कैबरे प्रदर्शनों का विकास उन नाइट क्लबों में होना है, जो अमरीका, यूरोपीय लैटिन अमरीकी और पूर्वी एशियाई देशों में चल रहे हैं। मसाज सेन्टरों और रिजोर्टों में चलनेवाला देह व्यापार और तेजी से फले-फूलेगा। पुराने फिल्मी गानों और लोकगीतों को स्त्री देह की चाशनी में लपेटकर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति आगे और जोर पकड़ेगी। आशा भोंसले जैसी सुगम संगीत की और सुभा मुद्गल जैसी शास्त्रीय संगीत की गायिकाएँ भी इस मैदान में उतर आई हैं।
केट मिलेट और अन्य कई आलोचकों ने अश्लीलता का स्त्रीवादी विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया है। इस सारे विवेचन की सीमा यह है कि वह अधिकांशतः लिखित साहित्य के सन्दर्भ में हुआ है। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के उच्च-प्रौद्यौगिकी युग में प्रचलित फीचर फिल्मों, गैर फीचर फिल्मों, टेलिविजन, टेबल एवं इंटरनेट प्रसारणों में अश्लीलता का सवाल नए सिरे से विवेचन की चुनौती उपस्थित करता है। जहाँ तक अवैध रूप से प्रसारित नग्न यौनाचार (पोर्नोग्राफी) का सवाल है, उसे सीधे कानूनन प्रतिबन्धित किया जा सकता है। वैसे प्रसारणों पर प्रतिबन्ध होता भी है। इनका निर्माण और प्रदर्शन समाज और कानून की निगाह से छिपकर किया जाता है। बच्चे और किशोर, जिनके ऊपर अश्लीलता के दुष्प्रभाव की सर्वाधिक चिन्ता की जाती है उनसे कुछ हद तक बचे रहे सकते हैं। लेकिन बाकी बचा जो कानूनसम्मत प्रसारण है, उसमें भी अश्लीलता का सवाल सुलझा हुआ नहीं है और अक्सर बहस का विषय बनता रहता है।
इधर पिछले कुछ वर्षों से फिल्मी तथा गैर फिल्मी नाच गानों के अलबमों और कुछ विज्ञापनों में स्त्री के शरीर की झटकेदार-मसालेदार नुमाइश भारतीय समाज के सन्दर्भ में अभूतपूर्व कही जाएगी। नग्न यौनाचार की हदों को छूता मसाला रमणियों का देह-प्रदर्शन कैसे भी कलात्मक और नैतिक मानदंडों से स्खलित, महज कामोत्तेजक होता है। सम्भवतः सौन्दर्य पहली बार इतना श्रीहीन और कुत्सित हुआ है। हालाँकि, साहित्य, स्थापत्य और चित्रकलाओं में बहुत पहले से स्त्री-शरीर और काम-चेष्टाओं का चित्रण पढ़ने-देखने को मिलता है, लेकिन नई लहर की विशिष्टता यह है उसमें शुरू से आखिर तक बाजारूपन तारी है। बाजारूपन के सभी मायनों के साथ, इस मायने में भी कि वह सबके ‘कंजप्शन’ के लिए होता है। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की क्रान्ति के चलते इसकी पहुँच समाज के हर तबके और हर उम्र के दर्शकों के लिए एक साथ है। इंटरनेट के जरिए कानूनन प्रतिबन्धित नग्न यौनाचार भी अब सर्वसुलभ है। यानी वैश्वीकरण केवल व्यापार का नहीं, देह-व्यापार का भी हो रहा है। भारत समेत प्रायः सभी आधुनिकता पूर्व समाजों में स्त्री-देह के प्रति भोगवादी बुद्धि की प्रधानता रही है। आधुनिक काल में उसके साथ मुनाफाखोर बुद्धि जुड़ गई है। पूँजीवादी व्यवस्था में हखियारों और नशीली वस्तुओं के साथ स्त्री देह भी मुनाफाखोरी का जबरदस्त जरिया है।
शर्त यही है कि प्रदर्शन जितना अश्लील होगा, मुनाफा भी उतना ही ज्यादा होगा। नग्न यौनाचार अगर अकूत मुनाफे का सौदा है तो इसीलिए कि उसमें अश्लीलता की कोई सीमा स्वीकार नहीं की जाती। नीली फिल्मों के अथाह समुद्र का विश्लेषण इस लेख का विषय नहीं है। यहाँ उस समुद्र के किनारों पर दिखाई देनेवाली अश्लीलता पर चर्चा की गई है। जाहिर है, जो किनारे पर है, उसका रिश्ता गहराइयों से है। किनारे पर खुला खेल खेलनेवाली स्त्रियाँ और उनके उद्यम को भारतीय समाज में आए खुलेपन का गुण बतानेवाले कतिपय फिल्मों के समाजशास्त्रियों को इस पर कड़ी आपत्ति होगी कि देह-प्रदर्शन को देह व्यापार (जिस्म फरोशी या वेश्यावृत्ति) से जोड़ा जाए। इस पर थोड़ा विचार कुछ देर बाद किया गया है कि आधुनिक देह-प्रदर्शन आधुनिक देह-व्यापार का ही एक रूप है और परम्परागत देह व्यापार से कहीं ज्यादा अनैतिक कर्म है।
स्त्री-देह की कानूनन प्रतिबन्धित और कानून सम्मत प्रदर्शन की परिघटना का स्रोत पूँजावादी अमरीका और पश्चिमी यूरोप के देश हैं। लैटिन अमरीका, अफ्रीका पूर्वी एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में तो इस परिघटना ने काफी पहले पहुँच बना ली थी, वैश्वीकरण की मुहिम के साथ भारत सहित बाकी के देशों में भी उसका तेजी से प्रवेश हुआ है। बहुलतावाद की बात करनेवाली उत्तर आधुनिक विचारधारा, उच्च पूँजीवाद जिसका व्यवस्थागत आधार है, में सभी समाजों और सभी उम्र के दर्शकों के लिए सुलभ एकरूप खुलापन परोसा जा रहा है। शायद आगे दस वर्ष भी न लगें जब भारत में भी फिल्मों और गैर फिल्मी नाच गानों के अलबमों में वैसी ही मैथुन मुद्राओं का प्रदर्शन होने लगे, जैसा हॉलीवुड, विकसित विश्व की अनेकानेक नाचमंडलियों और फैशन परेडों की प्रस्तुतियों में होता है। आगे चलकर कैबरे प्रदर्शनों का विकास उन नाइट क्लबों में होना है, जो अमरीका, यूरोपीय लैटिन अमरीकी और पूर्वी एशियाई देशों में चल रहे हैं। मसाज सेन्टरों और रिजोर्टों में चलनेवाला देह व्यापार और तेजी से फले-फूलेगा। पुराने फिल्मी गानों और लोकगीतों को स्त्री देह की चाशनी में लपेटकर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति आगे और जोर पकड़ेगी। आशा भोंसले जैसी सुगम संगीत की और सुभा मुद्गल जैसी शास्त्रीय संगीत की गायिकाएँ भी इस मैदान में उतर आई हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i