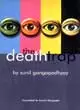|
सामाजिक >> आत्मप्रकाश आत्मप्रकाशसुनील गंगोपाध्याय
|
80 पाठक हैं |
|||||||
मध्यवर्गीय युवावर्ग के अंतर्मन का एक दस्तावेज
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘आत्मप्रकाश’ सुनील गंगोपाध्याय का पहला प्रकाशित उपन्यास है।
उपन्यास में वर्णित युवावर्ग सुनील-शेखर-अविनाश-सुविमल मानो वेदीहीन
पुरोहित हों जो पूजा-योग्य प्रतिमा की खोज में लगे हैं, वे मानो
बेरिकेड-विहीन विद्रोही हों, जो श्मशान के चक्कर काटते हैं, शराब-गांजा
पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मारा-मारी करते हैं। यह सब के एक आंतरिक रिक्तता
के दबाव के कारण करते हैं। उपन्यास के मुख्य पात्र सुनील गंगोपाध्याय के
जीवन में आयी तीनों ही नारियां गायत्री, मनीषा-यमुना उसके जीवन को आंदोलित
करती हैं। लेकिन छोटी उम्र की यमुना ही वह लड़की है जिसमें वह, बेशक नशे
की हालत में ही, पवित्र देवी के रूप में देखता है। यमुना भी उसे मिलती तो
नहीं, लेकिन वह उसके जीवन-क्रम को बदल देती है। यह बदलाव मोहभंग नहीं।
सुनील स्वयं अंत में कह उठता है-‘‘धरती को तनिक भी आघात न
पहुँचे, इसलिए धरती पर बहुत धीरे-धीरे पैर रखता हूँ।’’
मध्यवर्गीय युवावर्ग के अंतर्मन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है यह उपन्यास।
भूमिका
द्वितीय महायुद्ध के दौरान उसके तत्काल बाद बंगाल के मध्यवर्गीय समाज में
प्रचलित रीति-रिवाजों और प्रथाओं को अनेक दिशाओं के इतने आघात लगे कि उसकी
जड़े तक हिल गयीं। पांचवे दशक में पड़े भयंकर अकाल में मूक साक्षियों के
लिए उचित था कि वे इस जघन्य कांड के लिए नैतिक अपराध का बोध करें, लेकिन
वैसा हुआ नहीं। स्वयं अपनी आत्मरक्षा के लिए व्याकुल मध्यवर्गीय बंगाली
मानस का अपराधबोध सामाजिक सक्रियता में रूपांतरित नहीं हुआ है। हां,
बांग्ला उपन्यास, कहानी और नाटक उसके दर्शन अवश्य हुए। उसके तत्काल बाद ही
भंयकर खूनी सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें अनेक पुराने स्लोगनों को दफना
दिया गया। स्वतंत्रता मिली, पर भारत खंडित हो गया। घर-द्वारहीन अनगिनत
लोगों कि लिए स्वतंत्रता के उत्सव का कोई अर्थ नहीं रहा है। कई देशी
बैंकों में ताले लग गये। अनेक संस्कार, अनेक सपने टूट गये। दूसरे
विश्वयुद्ध से पहले ही प्रेम, साधना और निर्मल सपनों के काल में शाश्वत
नियम के अनुसार प्रेम, साधना और निर्मल सपनों में घुन लग गया था। जिसके
जन-जीवन को पूरी तरह छलनी कर दिया। इसका परिचय मिला महायुद्ध की ब्लैकआउट
की रातों में, भाई द्वारा भाई का गला काटने में। आदर्श की अनेक प्रतिमाओं
का रंग-रोगन और साज-सज्जा देखते-देखते धुल-पुंछ गये। प्रमोद कुमार सान्याल
(1905-1983) की युद्धकालीन कहानी ‘अंगार’ का अंतिम
अनुच्छेद
या संतोष कुमार घोष की ‘किनु गोलार गली’ या
ज्योतिरिंद्र नदी
की ‘मीरार दुपुर’ रचनाएं मानो यही एक बात कह रही हों
कि हमारा
बहुत कुछ खो गया है।
इसके प्रायः सौ साल पहले उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक में बांग्ला उपन्यास ने अपनी यात्रा शुरू की थी। उस समय इन उपन्यासों में जिस मध्यवर्ग का चित्रण हो रहा था, उस मध्यवर्ग ने अपनी सुरक्षा एवं स्थिति बनाये रखने के लिए अपने को आधुनिक भारतीय इतिहास के तांडव सरीखे प्रथम सैनिक-विद्रोह से विमुख रखा। बांग्ला साहित्य के प्रथम उपन्यास ‘आलालेर घरेर दुलाल’ (1858) में विक्टोरियन युग के मध्यवर्ग ने और कुछ नहीं खोजा। और कुछ चाहा था या खोजा था तो केवल पाश्चात्य शिक्षा द्वारा अनुमोदित व्यवहार तथा रीति-रिवाज-भद्रलोक (gentlemen) कैसे हुआ जाय। लेकिन केवल बांग्ला का प्रथम उपन्यास होने के कारण ही नहीं, ‘आलालेर घरेर दुलाल’ अपनी अन्य दो विशिष्टताओं के कारण भी स्वतंत्र महत्व का अधिकारी है। पहली विशिष्टता है इसका ऋजु गद्य, जो जीवन की औसत स्वाभाविकता को, टाइप चरित्रों को, सहज रूप में चित्रित कर सका। दूसरी विशिष्टता है आसपास के जीवन से जुड़े होना। इस उपन्यास के द्वारा ही पहली बार समझ में आया कि कहानियों के विषय हमारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं। बंकिमचंद्र (1838-1894) ने अपनी रचनाओं में गंभीर प्रश्नों और जीवन की व्याख्या को महत्व दिया। इसके सहायक थीं उनकी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि और गहरी प्रज्ञा, बंकिमचंद्र के प्रसंग में जिसका दूसरा नाम था कल्पना। यह सही है कि बंकिमचंद्र बंगाल के विक्टोरियनों की तरह नये उभरते हुए मध्य वर्ग के जागरुक प्रहरी थे।
यह भी सही है कि उनके विद्रोही पात्रों द्वारा अंत में अस्त्रत्याग किए जाने के कारण परवर्ती काल में उनकी पर्याप्त आलोचना भी हुई, जैसे आनंदमठ (1884), या चंद्रशेखर (1875) जिसमें विद्रोही नारियाँ प्रायश्चित करके घर लौट जाती है। साथ ही यह भी सही है कि दुविधा में पड़े भद्र पुरुष-चरित्रों के पास खड़ी हैं उनके ही द्वारा निर्मित और कल्पित महिलाएं जो जीवन के आवेश स्पंदित (Vibrant) है और जो नियति के साथ संबंध के बारे में कहती है कि-‘हम एक ही डाल के दो फूल थे, एक ही जंगल में हम खिले थे, हमें तोड़कर अलग क्यों किया ?’ या मृत्यु के सामने खड़ी रोहिणी (कृष्णकांतेर विल, 1878) जब कहती है- ‘मरूं क्यों’ ? तब समझ में आता है कि बंकिम की नायिकायें सुख-सुविधाओं की खातिर, किसी संस्कार या प्रथा को समझना चाहा था अपने रक्तमांस से, कामना और प्रेम से, अर्थात् शरीर और आत्मा दोनों से। यह बात केवल शैवलिनी या रोहिणी के प्रसंग में ही सत्य हो ऐसा नहीं यह बात पदमावती (कपालकुंडला, 1866), कुंद (विषवृक्ष, 1873), यहां तक कि इंदिरा (इंदिरा, 1873), के संबंध में भी सत्य है। दुखांत या सुखांत दोनों ही स्थितियों में बंकिम की नायिकाएं समान रूप से अपराजेय हैं, समान रूप से प्राणवंत हैं। उनके भद्र नायकों में अमरनाथ (रजनी 1877), केवल परम्परागत ट्रैजिक हीरो हो सो बात नहीं, वह विछिन्नता, अवसाद, दायित्व आदि की दृष्टि से आधुनिक चरित्रों का आगामी पात्र है। वह किसी भी चीज से अंत तक जुड़ नहीं पाया। ‘कृष्णकांतेर विल’ उपन्यास का गोविन्दलाल अपने असफल जीवन के अंत में सन्यास ले लेता है और ईश्वर की खोज में निकल पड़ता है। अमरनाथ कश्मीर चला जाता है। इन दोनों महाप्रस्थानों का अंतर विचारणीय है।
बंकिमचंद्र निसंदेह बहुत बड़े उपन्यासकार थे। किसी उपन्यास की श्रेष्ठता का मूल्याकन उसे उसके देशकाल की पृष्ठभूमि में रखकर ही किया जा सकता है। अपने मूल्यांकन उसे उसके जीवन में वे जिन समस्याओं का सामना करते हैं, उनका प्रभाव उनके उपन्यास के शिल्प पर भी पड़ता है। अमरनाथ जैसे चरित्र की समस्या का अंकन ‘रजनी’ उपन्यास की विशिष्ट टेकनीक के अतिरिक्त संभव न हो पाता। इसी प्रसंग में यदि हम रवीन्द्रनाथ के उपन्यासों पर विचार करें तो पाते हैं कि उनके सामने व्यक्ति की संपूर्ण सत्ता के संकट की समस्या प्रमुख थी। इस प्रसंग में सबसे पहले याद आती है विनोदनी (चोखरे बालि, 1903) की। विनोदनी की कहानी एक ऐसी नारी की कहानी है जो हर दृष्टि से एक ऐसे लंगडे सुविधावादी समाज में जहां नारी के मूल्यांकन का एकमात्र मापदंड सम्पत्ति-चेतना हो, अपनी प्रतिभा की दृष्टि से बंकिमचंद्र और रवीन्द्रनाथ में एक बड़ा है न दूसरा छो़टा। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से रवीन्द्रनाथ को अनुकूल परिस्थितियां मिली थीं। वर्तमान शताब्दी के पहले दशक में लार्ड कर्जन की कर्जनी तलवार के विरुद्ध बंगाल में अंग्रेज सरकार विरोधी जिस स्वदेशी का सूत्रपात हुआ था, रवींद्रनाथ उसके प्रत्यक्ष भागीदार थे और प्रत्यक्ष भागीदार होने के फलस्परूप उन्होंने बहुत कुछ स्वयं निकट से देखा और जाना था। बंकिमचंद्र को संभवतया उनका आभास ही मिला था, पर वह अस्पष्ट था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्यवर्ग के सामने उपस्थित संपूर्ण संकट की ओर, उसके अभिप्राय और सिद्धप्राय और सिद्धप्राप्ति के बीच दिखाई पड़ने लगती वाली मूलभूत असंगति की ओर रवींन्द्रनाथ ने महाकाव्य जैसे अपने उपन्यास गोरा (1910) में सर्वप्रथम उंगली उठायी।
इस काम का आरंभ वे इससे पहले रचित एक अत्यंत मार्मिक कहानी ‘मेघ’ ओ रौद्र’ (1894) में कर चुके थे। भारतीयत्व का मतलब ब्राहमणत्व या हिंदूत्व नहीं है। भारतीयत्व विश्वामानवत्व का एक आत्मनिर्भर भारतीय अंश है। नायक गोरा कैसे इस तत्व को उपलब्ध करता है, यही इस उपन्यास का कथ्य है। गोरा, घने-बहरे (1915) और चार अध्याय (1934), इन तीनों उपन्यासों के पीछे थी रवींद्रनाथ की स्वदेश संबंधी तीव्र उत्कंठा। ‘घरे बाइरे’ की लेखनाविधि में ही ‘चतुरंग’ का सजृन हुआ। केवल विशिष्ट शिल्प की दृष्टि से ही नहीं-निराकार के साथ अन्वित होने की लालसा से शचीश और जीवन के साथ अन्वित होने की लालसा से दामिनी-ये दोनों ही अपनी-अपनी समानांतर यात्रा के द्वारा इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि ईश्वर हो या जीवन हम किसी को भी क्यों न खोजें, इस खोज में उस तथ्य को पाने की चेष्टा और साधना ही प्रमुख होती है। इसी दृष्टि से यह उपन्यास बेजोड़ है। आश्यचर्यजनक चरित्र था दामिनी का-उसने उत्तर की हवा को रत्तीभर महत्त्व नहीं दिया। रवींन्द्रनाथ की सभी नायिकाओं ने-वह चाहे विनोदिनी हो या दामिनी या फिर ‘योगायोग’ की कुमु, सबने अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग ढंग से अपनी-अपनी सत्ता की अनावृत्त शुद्धता को खोजने का प्रयत्न किया था। ‘घरे बाइरे’ की विमला को यह खोज करनी पडी़ थी ट्रैजेडी के रक्ताभ पथ को रौंदते हुए। पूरे उपन्यास में उस जैसा जीवंत व्यक्तित्व और कोई है क्या !
उपन्यासकार रवींन्द्रनाथ जब बंगला साहित्य के आकाश में देदिप्यमान थे, तभी उपन्यास विधा में शरदचंद्र का प्रादुर्भव हुआ। बंकिमचंद्र या रवींद्रनाथ जैसा तात्विक या बौद्धिक वातावरण शरतचंद्र के उपन्यासों में नहीं था। जहाँ कही उपन्यासकार ने वैसा वातावरण बनाने का प्रयत्न किया, वहां असफल रहा, जैसे ‘शेष प्रश्न’ (1931) में। यह उनका क्षेत्र नहीं था, लेकिन व्यक्ति के हृदय की परतों को खोलकर रखने का कौशल उनमें बेजोड़ था। उनके उपन्यासों का कथानक सीधा-साधा होता था और पात्र ग्रामीण मध्यवर्ग के। उनकी मानसिकता भी वैसी ही होती थी। लेकिन उनके उपन्यास ‘निष्कृति’ (1917) के दिलीप कुमार राय द्वारा किये गये अंग्रेजी अनुवाद ‘Deliverance’ की भूमिका में रवींन्द्रनाथ के सामन्य रूप से उनके बारे में जो लिखा था, वह पूरी तरह सही है-
‘‘He has imparted a new power to our language and in his stories has shed the light of a fresh vision upon the too familiar region of Bengal’s heart revealing the living significance of the obscure trifles of the people’s personality , ’’
शरतचंद्र द्वारा निर्मित पात्र श्रीकांत-इंद्रनाथ-जीवानंद और राजलक्ष्मी-अन्नदा-किरणमयी-नारायणी आदि ने बंगाली मानस के अंतःपुर में स्थान बना दिया। मानवीय अस्तित्व का सारतत्व है उसका प्रेम-यही बताने के लिए ही वे आये थे और अपना यह काम उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से पूरा किया।
प्रथम महायुद्ध के बाद रचित शरतचंद्र का ‘श्रीकांत’ (1917-1923) और रवींन्द्रनाथ का ‘शेषेर कविता’ एक ही तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। ‘श्रीकांत’ का नायक श्रीकांत या शेषर कविता’ का नायक अमित, दोनों में से कोई भी गोरा के निकट नहीं पहुंचता। दोनों में से किसी की कोई निश्चित पृष्ठभूमि नहीं है। अमित की पृष्ठभूमि है शिलांग का पहाड़ रवींन्द्रनाथ का प्रिय कोई समतल क्षेत्र नहीं। बंगभूमि तो नहीं ही। श्रीकांत सदा घूमता रहता है, उसके रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं। करने का भी कुछ नहीं। उसके पास न किसी जीत का गौरव है, न किसी हार की ट्रैजिक महिमा। ‘शेषेर कविता’ का अमित भी क्या बहुत कुछ ऐसा ही नहीं है ! असम्पृक्त, असंलग्न अमित की नगरीय-दीप्ति में शून्य उद्देश्यहीन है। वह अपनी बातों के प्रेम में ही डूबा रहता है। उसकी बातें टक्साली मुद्रा जैसी जरूर हैं पर वह अपनी बातों के प्रेम में ही डूबा रहता है। और इस कारण उन पर संदेह होता है। कहां आदर्शनिष्ठ गोरा और कहां वाणीनिष्ठ अमित !
इस बीच प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सारे संसार में आने वाली मंदी की चपेट में खो गया बंगाली भद्रलोक का वह वर्ग-स्वप्न। ‘कल्लोल’ पत्रिका (1923) हर दृष्टि से इसी मानसिकता की उपज थी।
उसका विद्रोही स्वर कितना ही सारहीन क्यों न रहा हो पर यह तो सच था कि उसके प्रमुख लेखक मध्यवर्ग में पड़ती दरारों और उसकी असहायता के प्रति सचेत थे। सन् 1884 में बंकिमचंद्र ने ‘प्रचार’ पत्रिका में मध्यवर्ग के हाथों में सामाजिक नेतृत्व आने पर हर्ष व्यक्त किया था। उसके बाद 43 साल निकल गये। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका। ‘कल्लोल’ के सन् 1927 के फरवरी अंक में बंगाल के मध्यवर्ग का जो चित्र प्राप्त होता है उससे स्पष्ट है कि बंकिमचंद्र उस हर्ष का कारण बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। साफ समझ में आता है कि मध्यवर्ग के परिवारों का टूटना और उनका रूपांतर होना समांतर घटना के रूप में घटित हो रहे थे। नियति के चैलेंज को स्वीकार करने वाले नायक दुर्लभ हो गये। यद्यपि कुछ लेखकों को न्यूट हमसुन और मैक्सिम गोर्की ने प्रभावित किया था, तथापि वह प्रभाव फैशन मात्र था। सच पूछा जाय तो प्रेमेंद मित्र (1904-1988) की कहानियों में ही मध्यवर्ग के मानस की भविष्यहीनता और अंधकार की स्पष्ट स्वीकृति देखने को मिलती है। इस युग के वास्तविक प्रतिनिधि माणिक बंद्योपाध्याय के उपन्यास ‘पुतुल नाचेर इतिकथा’ का शशि अपने प्रेम और सम्पूर्ण अस्तित्व को परिवेशगत नियति और व्यक्तिगत नियति के नागपास से मुक्त करके बाहर नहीं ला सका।
आकांक्षा की आग जलाकर भी जो लोग जला न सके, जो उस आग के ताप में अपनी शीतलता को गला न सके-शशि ऐसे युवावर्ग का प्रतिनिधि था। जब व्यक्ति स्वयं अपने भविष्य का रचयिता हो, क्षेत्र चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक-और नाना रूपों में मार खा रहा हो, शशि ऐसे ही समय (युग) का प्रतिनिधि था। इसी समयावधि में लिखा गया विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय (1894-1950) का ‘पाथेर पांचाली’ (1923)। आश्चर्य की बात है कि जिस तरह युवक शशि ने जीवन की जटिलता के इतिहास को जाना और जानते-जानते जिस तरह उसे अपने सारे संकल्पों का उदासीन गेरुआ काल-स्त्रोत में प्रवाहित कर देना पड़ा उसी तरह ‘पाथेर पांचाली’ के नायक अपु ने भी जाना कि धरती जिस ममता को विकीर्ण करती है और मनुष्य जिस ममता को देता है उसमें ही निहित है अशेष का इंगित। माणिक मानों वैज्ञानिक हों और विभूतिभूषण दार्शनिक। दूसरी ओर ताराशंकर बंद्योपाध्याय (1998-1971) ने समाज और व्यक्ति की द्वन्द्वात्मक समग्रता को समझना चाहा था यह बात उसके असाधारण चिंतन-समृद्ध सामाजिक उपन्यास’ गणदेवता (1942) ‘पंचग्राम’ (1943) के बारे में जितनी सत्य है उतनी ही उनके मुख्य आंचलिक उपन्यास ‘हांसुली बांकेर उपकथा’ (1947) के बारे में भी सत्य है। व्यक्ति को अपने जीवन में होना (Becoming)- यह बात उनके उपन्यास ‘कवि’ (1942) में बड़े सार्थक रूप में प्रस्फुटित हुई है। इस प्रसंग में एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करूं। हम लोगों ने ताराशंकर के जिन उपन्यासों की चर्चा की उनके अतिरिक्त और कई उपन्यासों का भी उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन उनमें से किसी का विषय नगर से संबंधित नहीं है, उनके नायक किसी नगरीय परिवेश के जीव नहीं हैं। यह नहीं कि कलकत्ता की पृष्ठभूमि में बाकायदा मध्यवर्ग के किसी व्यक्ति को केंद्र में रहकर ताराशंकर ने उपन्यास न लिखा, लेकिन उन उपन्यासों के पढ़ने से यह साफ समझ में आता है कि ऐसी रचना करते समय वे बंधा-बंधा अनुभव कर रहे हैं, सहज नहीं हो पाये हैं।
कुछ-कुछ ऐसी ही स्थिति हमें ताराशंकर के परवर्ती उपन्यासकार सतीनाथ भादुडी़ की रचनाओं में भी दिखाई पड़ती है। उनका कोई भी उपन्यास कलकत्ता या किसी और बड़े शहर की पृष्ठभूमि में नहीं लिखा गया है। मफस्सल के एक मध्यवर्गीय परिवार को लेकर उन्होंने एक साधारण उपन्यास ‘दिग्भ्रांत’ (1966) की रचना की थी। ‘ढोंडाइ चरितमानस’ (1949) या ‘जागरी*(1946) की सफलता की तुलना में पारिवारिक संकट के उपन्यास दिग्भ्रांत की सफलता तनिक भी मलिन नहीं होती। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इसी काल के एक और महत्त्वपूर्ण उपन्यासकार अभियभूषण मजुमदार ने भी कलकत्ता की पृष्ठभूमि या विशुद्ध नगरीय पृष्ठभूमि में किसी उपन्यास की रचना नहीं की। यह स्थिति हमें अलग हटकर सोचने को बाध्य करती है। बांग्ला के प्रमुख उपन्यासकारों में एक मात्र रवींन्द्रनाथ ऐसे थे जिनकी औपन्यासिक चेतना नगरीय थी। बंकिमचंद्र के पांच सामाजिक-पारिवारिक उपन्यासों में एकमात्र ‘रजनी’ की पृष्ठभूमि कलकत्ता है, शेष सभी मफस्सल में स्थिति हैं। ‘कल्लोल’ गोष्ठी के लेखकों का जो वर्ग विदेशी हवा से पाल को चलाने को व्याकुल था, उसके सामने कलकत्ता-केंद्रिक होने के सिवा कोई और चारा नहीं था। अपनी व्यक्तिगत बौद्धिकता के कारण, अपने कथ्य के दबाव के फलस्वरूप जिन्हें गाँव छोड़कर कलकत्ता को चुनना पड़ा था, वे थे माणिक बंद्योपाध्याय। उनके पात्रों की जटिल मानसिकता के लिए कलकत्ता की पृष्ठभूमि ही अधिक उपयुक्त थी।
‘शहरतली’ उपन्यास इसका प्रमाण है।
द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद कलकत्ता के मध्यवर्गीय लोगों के जीवन में अनेक अवसादों का उदय हुआ, अनेक आशाएं खंडित हुईं। इतने दिनों तक घर और बाहर को लेकर तिल-तिलकर गढ़े गये सपने टुकड़े-टुकड़े होकर धूल-धुसरित हो गये। टूटे सपने तेज धारवाले कांच के टुकड़ों की तरह केवल खून बहाते और पीड़ा बढा़ते हैं। लोगों को लगा कि उस कठोर वास्तविकता से नजर घुमाकर यदि अदूर या सुदूर अतीत की ओर देखा जा सके यदि ऐतिहासिक रोमांस को थोड़ा रंग-रोगन लगाकर लौटाया जा सके तो बुरा क्या है ? इस काल में अनेक शक्तिशाली उपन्याकारों ने इस तरह के उपन्यासों की रचना की। ताराशंकर ने ‘राधा’ और ‘गन्ना’ बेगम’, विभूतिभूषण ने ‘इच्छामती’, प्रमथनाथ बिशी (1901-1965) ने ‘केरी’ साहबेर मुंशी’ एवं विमल मित्र ने ‘बेगम मेरी बिस्वास’ उपन्यास लिखे, तथापि कलकत्ता शहर में एक उपन्यासकार को जिस चैलेंज का सामना करना पड़ता है, उसका सामना वे नहीं कर पाये। ‘हे हृदय मूल फैला दो टूटे पाषाणों में-यह एक वयोवृद्ध का कथन भी है एक उपन्यासकार का अनचाहा संकल्प भी। इसी को लेकर लिखा गया है ताराशंकर का ‘झड़ ओ झरा पाता’ व माणिक बंद्योपाध्याय का ‘चिह्न’ सन् 1946 की कलकत्ता का धधकती पृष्ठभूमि में। किंतु इस अग्निकांड की सारी ज्योति 16 अगस्त के छिन्नमस्तक कलकत्ता के काले वीभत्स धुएं में मलिन पड़ गयी।
बहुत कुछ खोना पड़ा, लेकिन सबसे दुखद और मंहगा पड़ा, सपनों को खोना। इस शताब्दी के पांचवें और छठे दशकों में जिन लोगों ने उपन्यास लिखे उन्होंने मध्यवर्ग की मानसिकता के बीच खडे़ होकर कुछ खोजने का प्रयत्न किया। वे सभी शक्तिशाली गद्य लेखक थे।
नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया द्वारा इस उपन्यास का हिंदी साहित्य ग्यारह भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है।
वे द्वितीय महायुद्ध या उसके तत्काल के बाद के कलकत्ता से परिचित थे। विमल कर का ‘देवाल’ असीम राय का ‘एकालेर कथा’, नरेन्द्रनाथ मित्र का ‘चेनामहल’, संतोषकुमार घोष का ‘किंनु गोलार गली’, ज्योतिरिंद्र नंदी (1917-1975) का ‘बारो घर एक उठान’ आदि सभी उपन्यासों के पात्र यदि विशिष्ट बन पाये हैं तो केवल इस माने में कि इनमें से कोई भी उन्नीसवीं सदी के मध्यवर्ग के पात्रों से मिले उत्तराधिकार की रक्षा के लिए चिंतित नहीं था, होने का कोई कारण भी नहीं था। और इतिहास ने भी अपने नियम के अनुसार उनके हाथों में पकड़ा दी खाली झोली। उसमें जो कुछ पुरानी मुद्राएं थीं भी, उन्हें अब उनके बाजार में भुनाया नहीं जा सकता।
इसके प्रायः सौ साल पहले उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक में बांग्ला उपन्यास ने अपनी यात्रा शुरू की थी। उस समय इन उपन्यासों में जिस मध्यवर्ग का चित्रण हो रहा था, उस मध्यवर्ग ने अपनी सुरक्षा एवं स्थिति बनाये रखने के लिए अपने को आधुनिक भारतीय इतिहास के तांडव सरीखे प्रथम सैनिक-विद्रोह से विमुख रखा। बांग्ला साहित्य के प्रथम उपन्यास ‘आलालेर घरेर दुलाल’ (1858) में विक्टोरियन युग के मध्यवर्ग ने और कुछ नहीं खोजा। और कुछ चाहा था या खोजा था तो केवल पाश्चात्य शिक्षा द्वारा अनुमोदित व्यवहार तथा रीति-रिवाज-भद्रलोक (gentlemen) कैसे हुआ जाय। लेकिन केवल बांग्ला का प्रथम उपन्यास होने के कारण ही नहीं, ‘आलालेर घरेर दुलाल’ अपनी अन्य दो विशिष्टताओं के कारण भी स्वतंत्र महत्व का अधिकारी है। पहली विशिष्टता है इसका ऋजु गद्य, जो जीवन की औसत स्वाभाविकता को, टाइप चरित्रों को, सहज रूप में चित्रित कर सका। दूसरी विशिष्टता है आसपास के जीवन से जुड़े होना। इस उपन्यास के द्वारा ही पहली बार समझ में आया कि कहानियों के विषय हमारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं। बंकिमचंद्र (1838-1894) ने अपनी रचनाओं में गंभीर प्रश्नों और जीवन की व्याख्या को महत्व दिया। इसके सहायक थीं उनकी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि और गहरी प्रज्ञा, बंकिमचंद्र के प्रसंग में जिसका दूसरा नाम था कल्पना। यह सही है कि बंकिमचंद्र बंगाल के विक्टोरियनों की तरह नये उभरते हुए मध्य वर्ग के जागरुक प्रहरी थे।
यह भी सही है कि उनके विद्रोही पात्रों द्वारा अंत में अस्त्रत्याग किए जाने के कारण परवर्ती काल में उनकी पर्याप्त आलोचना भी हुई, जैसे आनंदमठ (1884), या चंद्रशेखर (1875) जिसमें विद्रोही नारियाँ प्रायश्चित करके घर लौट जाती है। साथ ही यह भी सही है कि दुविधा में पड़े भद्र पुरुष-चरित्रों के पास खड़ी हैं उनके ही द्वारा निर्मित और कल्पित महिलाएं जो जीवन के आवेश स्पंदित (Vibrant) है और जो नियति के साथ संबंध के बारे में कहती है कि-‘हम एक ही डाल के दो फूल थे, एक ही जंगल में हम खिले थे, हमें तोड़कर अलग क्यों किया ?’ या मृत्यु के सामने खड़ी रोहिणी (कृष्णकांतेर विल, 1878) जब कहती है- ‘मरूं क्यों’ ? तब समझ में आता है कि बंकिम की नायिकायें सुख-सुविधाओं की खातिर, किसी संस्कार या प्रथा को समझना चाहा था अपने रक्तमांस से, कामना और प्रेम से, अर्थात् शरीर और आत्मा दोनों से। यह बात केवल शैवलिनी या रोहिणी के प्रसंग में ही सत्य हो ऐसा नहीं यह बात पदमावती (कपालकुंडला, 1866), कुंद (विषवृक्ष, 1873), यहां तक कि इंदिरा (इंदिरा, 1873), के संबंध में भी सत्य है। दुखांत या सुखांत दोनों ही स्थितियों में बंकिम की नायिकाएं समान रूप से अपराजेय हैं, समान रूप से प्राणवंत हैं। उनके भद्र नायकों में अमरनाथ (रजनी 1877), केवल परम्परागत ट्रैजिक हीरो हो सो बात नहीं, वह विछिन्नता, अवसाद, दायित्व आदि की दृष्टि से आधुनिक चरित्रों का आगामी पात्र है। वह किसी भी चीज से अंत तक जुड़ नहीं पाया। ‘कृष्णकांतेर विल’ उपन्यास का गोविन्दलाल अपने असफल जीवन के अंत में सन्यास ले लेता है और ईश्वर की खोज में निकल पड़ता है। अमरनाथ कश्मीर चला जाता है। इन दोनों महाप्रस्थानों का अंतर विचारणीय है।
बंकिमचंद्र निसंदेह बहुत बड़े उपन्यासकार थे। किसी उपन्यास की श्रेष्ठता का मूल्याकन उसे उसके देशकाल की पृष्ठभूमि में रखकर ही किया जा सकता है। अपने मूल्यांकन उसे उसके जीवन में वे जिन समस्याओं का सामना करते हैं, उनका प्रभाव उनके उपन्यास के शिल्प पर भी पड़ता है। अमरनाथ जैसे चरित्र की समस्या का अंकन ‘रजनी’ उपन्यास की विशिष्ट टेकनीक के अतिरिक्त संभव न हो पाता। इसी प्रसंग में यदि हम रवीन्द्रनाथ के उपन्यासों पर विचार करें तो पाते हैं कि उनके सामने व्यक्ति की संपूर्ण सत्ता के संकट की समस्या प्रमुख थी। इस प्रसंग में सबसे पहले याद आती है विनोदनी (चोखरे बालि, 1903) की। विनोदनी की कहानी एक ऐसी नारी की कहानी है जो हर दृष्टि से एक ऐसे लंगडे सुविधावादी समाज में जहां नारी के मूल्यांकन का एकमात्र मापदंड सम्पत्ति-चेतना हो, अपनी प्रतिभा की दृष्टि से बंकिमचंद्र और रवीन्द्रनाथ में एक बड़ा है न दूसरा छो़टा। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से रवीन्द्रनाथ को अनुकूल परिस्थितियां मिली थीं। वर्तमान शताब्दी के पहले दशक में लार्ड कर्जन की कर्जनी तलवार के विरुद्ध बंगाल में अंग्रेज सरकार विरोधी जिस स्वदेशी का सूत्रपात हुआ था, रवींद्रनाथ उसके प्रत्यक्ष भागीदार थे और प्रत्यक्ष भागीदार होने के फलस्परूप उन्होंने बहुत कुछ स्वयं निकट से देखा और जाना था। बंकिमचंद्र को संभवतया उनका आभास ही मिला था, पर वह अस्पष्ट था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्यवर्ग के सामने उपस्थित संपूर्ण संकट की ओर, उसके अभिप्राय और सिद्धप्राय और सिद्धप्राप्ति के बीच दिखाई पड़ने लगती वाली मूलभूत असंगति की ओर रवींन्द्रनाथ ने महाकाव्य जैसे अपने उपन्यास गोरा (1910) में सर्वप्रथम उंगली उठायी।
इस काम का आरंभ वे इससे पहले रचित एक अत्यंत मार्मिक कहानी ‘मेघ’ ओ रौद्र’ (1894) में कर चुके थे। भारतीयत्व का मतलब ब्राहमणत्व या हिंदूत्व नहीं है। भारतीयत्व विश्वामानवत्व का एक आत्मनिर्भर भारतीय अंश है। नायक गोरा कैसे इस तत्व को उपलब्ध करता है, यही इस उपन्यास का कथ्य है। गोरा, घने-बहरे (1915) और चार अध्याय (1934), इन तीनों उपन्यासों के पीछे थी रवींद्रनाथ की स्वदेश संबंधी तीव्र उत्कंठा। ‘घरे बाइरे’ की लेखनाविधि में ही ‘चतुरंग’ का सजृन हुआ। केवल विशिष्ट शिल्प की दृष्टि से ही नहीं-निराकार के साथ अन्वित होने की लालसा से शचीश और जीवन के साथ अन्वित होने की लालसा से दामिनी-ये दोनों ही अपनी-अपनी समानांतर यात्रा के द्वारा इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि ईश्वर हो या जीवन हम किसी को भी क्यों न खोजें, इस खोज में उस तथ्य को पाने की चेष्टा और साधना ही प्रमुख होती है। इसी दृष्टि से यह उपन्यास बेजोड़ है। आश्यचर्यजनक चरित्र था दामिनी का-उसने उत्तर की हवा को रत्तीभर महत्त्व नहीं दिया। रवींन्द्रनाथ की सभी नायिकाओं ने-वह चाहे विनोदिनी हो या दामिनी या फिर ‘योगायोग’ की कुमु, सबने अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग ढंग से अपनी-अपनी सत्ता की अनावृत्त शुद्धता को खोजने का प्रयत्न किया था। ‘घरे बाइरे’ की विमला को यह खोज करनी पडी़ थी ट्रैजेडी के रक्ताभ पथ को रौंदते हुए। पूरे उपन्यास में उस जैसा जीवंत व्यक्तित्व और कोई है क्या !
उपन्यासकार रवींन्द्रनाथ जब बंगला साहित्य के आकाश में देदिप्यमान थे, तभी उपन्यास विधा में शरदचंद्र का प्रादुर्भव हुआ। बंकिमचंद्र या रवींद्रनाथ जैसा तात्विक या बौद्धिक वातावरण शरतचंद्र के उपन्यासों में नहीं था। जहाँ कही उपन्यासकार ने वैसा वातावरण बनाने का प्रयत्न किया, वहां असफल रहा, जैसे ‘शेष प्रश्न’ (1931) में। यह उनका क्षेत्र नहीं था, लेकिन व्यक्ति के हृदय की परतों को खोलकर रखने का कौशल उनमें बेजोड़ था। उनके उपन्यासों का कथानक सीधा-साधा होता था और पात्र ग्रामीण मध्यवर्ग के। उनकी मानसिकता भी वैसी ही होती थी। लेकिन उनके उपन्यास ‘निष्कृति’ (1917) के दिलीप कुमार राय द्वारा किये गये अंग्रेजी अनुवाद ‘Deliverance’ की भूमिका में रवींन्द्रनाथ के सामन्य रूप से उनके बारे में जो लिखा था, वह पूरी तरह सही है-
‘‘He has imparted a new power to our language and in his stories has shed the light of a fresh vision upon the too familiar region of Bengal’s heart revealing the living significance of the obscure trifles of the people’s personality , ’’
शरतचंद्र द्वारा निर्मित पात्र श्रीकांत-इंद्रनाथ-जीवानंद और राजलक्ष्मी-अन्नदा-किरणमयी-नारायणी आदि ने बंगाली मानस के अंतःपुर में स्थान बना दिया। मानवीय अस्तित्व का सारतत्व है उसका प्रेम-यही बताने के लिए ही वे आये थे और अपना यह काम उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से पूरा किया।
प्रथम महायुद्ध के बाद रचित शरतचंद्र का ‘श्रीकांत’ (1917-1923) और रवींन्द्रनाथ का ‘शेषेर कविता’ एक ही तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। ‘श्रीकांत’ का नायक श्रीकांत या शेषर कविता’ का नायक अमित, दोनों में से कोई भी गोरा के निकट नहीं पहुंचता। दोनों में से किसी की कोई निश्चित पृष्ठभूमि नहीं है। अमित की पृष्ठभूमि है शिलांग का पहाड़ रवींन्द्रनाथ का प्रिय कोई समतल क्षेत्र नहीं। बंगभूमि तो नहीं ही। श्रीकांत सदा घूमता रहता है, उसके रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं। करने का भी कुछ नहीं। उसके पास न किसी जीत का गौरव है, न किसी हार की ट्रैजिक महिमा। ‘शेषेर कविता’ का अमित भी क्या बहुत कुछ ऐसा ही नहीं है ! असम्पृक्त, असंलग्न अमित की नगरीय-दीप्ति में शून्य उद्देश्यहीन है। वह अपनी बातों के प्रेम में ही डूबा रहता है। उसकी बातें टक्साली मुद्रा जैसी जरूर हैं पर वह अपनी बातों के प्रेम में ही डूबा रहता है। और इस कारण उन पर संदेह होता है। कहां आदर्शनिष्ठ गोरा और कहां वाणीनिष्ठ अमित !
इस बीच प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सारे संसार में आने वाली मंदी की चपेट में खो गया बंगाली भद्रलोक का वह वर्ग-स्वप्न। ‘कल्लोल’ पत्रिका (1923) हर दृष्टि से इसी मानसिकता की उपज थी।
उसका विद्रोही स्वर कितना ही सारहीन क्यों न रहा हो पर यह तो सच था कि उसके प्रमुख लेखक मध्यवर्ग में पड़ती दरारों और उसकी असहायता के प्रति सचेत थे। सन् 1884 में बंकिमचंद्र ने ‘प्रचार’ पत्रिका में मध्यवर्ग के हाथों में सामाजिक नेतृत्व आने पर हर्ष व्यक्त किया था। उसके बाद 43 साल निकल गये। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका। ‘कल्लोल’ के सन् 1927 के फरवरी अंक में बंगाल के मध्यवर्ग का जो चित्र प्राप्त होता है उससे स्पष्ट है कि बंकिमचंद्र उस हर्ष का कारण बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। साफ समझ में आता है कि मध्यवर्ग के परिवारों का टूटना और उनका रूपांतर होना समांतर घटना के रूप में घटित हो रहे थे। नियति के चैलेंज को स्वीकार करने वाले नायक दुर्लभ हो गये। यद्यपि कुछ लेखकों को न्यूट हमसुन और मैक्सिम गोर्की ने प्रभावित किया था, तथापि वह प्रभाव फैशन मात्र था। सच पूछा जाय तो प्रेमेंद मित्र (1904-1988) की कहानियों में ही मध्यवर्ग के मानस की भविष्यहीनता और अंधकार की स्पष्ट स्वीकृति देखने को मिलती है। इस युग के वास्तविक प्रतिनिधि माणिक बंद्योपाध्याय के उपन्यास ‘पुतुल नाचेर इतिकथा’ का शशि अपने प्रेम और सम्पूर्ण अस्तित्व को परिवेशगत नियति और व्यक्तिगत नियति के नागपास से मुक्त करके बाहर नहीं ला सका।
आकांक्षा की आग जलाकर भी जो लोग जला न सके, जो उस आग के ताप में अपनी शीतलता को गला न सके-शशि ऐसे युवावर्ग का प्रतिनिधि था। जब व्यक्ति स्वयं अपने भविष्य का रचयिता हो, क्षेत्र चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक-और नाना रूपों में मार खा रहा हो, शशि ऐसे ही समय (युग) का प्रतिनिधि था। इसी समयावधि में लिखा गया विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय (1894-1950) का ‘पाथेर पांचाली’ (1923)। आश्चर्य की बात है कि जिस तरह युवक शशि ने जीवन की जटिलता के इतिहास को जाना और जानते-जानते जिस तरह उसे अपने सारे संकल्पों का उदासीन गेरुआ काल-स्त्रोत में प्रवाहित कर देना पड़ा उसी तरह ‘पाथेर पांचाली’ के नायक अपु ने भी जाना कि धरती जिस ममता को विकीर्ण करती है और मनुष्य जिस ममता को देता है उसमें ही निहित है अशेष का इंगित। माणिक मानों वैज्ञानिक हों और विभूतिभूषण दार्शनिक। दूसरी ओर ताराशंकर बंद्योपाध्याय (1998-1971) ने समाज और व्यक्ति की द्वन्द्वात्मक समग्रता को समझना चाहा था यह बात उसके असाधारण चिंतन-समृद्ध सामाजिक उपन्यास’ गणदेवता (1942) ‘पंचग्राम’ (1943) के बारे में जितनी सत्य है उतनी ही उनके मुख्य आंचलिक उपन्यास ‘हांसुली बांकेर उपकथा’ (1947) के बारे में भी सत्य है। व्यक्ति को अपने जीवन में होना (Becoming)- यह बात उनके उपन्यास ‘कवि’ (1942) में बड़े सार्थक रूप में प्रस्फुटित हुई है। इस प्रसंग में एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करूं। हम लोगों ने ताराशंकर के जिन उपन्यासों की चर्चा की उनके अतिरिक्त और कई उपन्यासों का भी उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन उनमें से किसी का विषय नगर से संबंधित नहीं है, उनके नायक किसी नगरीय परिवेश के जीव नहीं हैं। यह नहीं कि कलकत्ता की पृष्ठभूमि में बाकायदा मध्यवर्ग के किसी व्यक्ति को केंद्र में रहकर ताराशंकर ने उपन्यास न लिखा, लेकिन उन उपन्यासों के पढ़ने से यह साफ समझ में आता है कि ऐसी रचना करते समय वे बंधा-बंधा अनुभव कर रहे हैं, सहज नहीं हो पाये हैं।
कुछ-कुछ ऐसी ही स्थिति हमें ताराशंकर के परवर्ती उपन्यासकार सतीनाथ भादुडी़ की रचनाओं में भी दिखाई पड़ती है। उनका कोई भी उपन्यास कलकत्ता या किसी और बड़े शहर की पृष्ठभूमि में नहीं लिखा गया है। मफस्सल के एक मध्यवर्गीय परिवार को लेकर उन्होंने एक साधारण उपन्यास ‘दिग्भ्रांत’ (1966) की रचना की थी। ‘ढोंडाइ चरितमानस’ (1949) या ‘जागरी*(1946) की सफलता की तुलना में पारिवारिक संकट के उपन्यास दिग्भ्रांत की सफलता तनिक भी मलिन नहीं होती। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इसी काल के एक और महत्त्वपूर्ण उपन्यासकार अभियभूषण मजुमदार ने भी कलकत्ता की पृष्ठभूमि या विशुद्ध नगरीय पृष्ठभूमि में किसी उपन्यास की रचना नहीं की। यह स्थिति हमें अलग हटकर सोचने को बाध्य करती है। बांग्ला के प्रमुख उपन्यासकारों में एक मात्र रवींन्द्रनाथ ऐसे थे जिनकी औपन्यासिक चेतना नगरीय थी। बंकिमचंद्र के पांच सामाजिक-पारिवारिक उपन्यासों में एकमात्र ‘रजनी’ की पृष्ठभूमि कलकत्ता है, शेष सभी मफस्सल में स्थिति हैं। ‘कल्लोल’ गोष्ठी के लेखकों का जो वर्ग विदेशी हवा से पाल को चलाने को व्याकुल था, उसके सामने कलकत्ता-केंद्रिक होने के सिवा कोई और चारा नहीं था। अपनी व्यक्तिगत बौद्धिकता के कारण, अपने कथ्य के दबाव के फलस्वरूप जिन्हें गाँव छोड़कर कलकत्ता को चुनना पड़ा था, वे थे माणिक बंद्योपाध्याय। उनके पात्रों की जटिल मानसिकता के लिए कलकत्ता की पृष्ठभूमि ही अधिक उपयुक्त थी।
‘शहरतली’ उपन्यास इसका प्रमाण है।
द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद कलकत्ता के मध्यवर्गीय लोगों के जीवन में अनेक अवसादों का उदय हुआ, अनेक आशाएं खंडित हुईं। इतने दिनों तक घर और बाहर को लेकर तिल-तिलकर गढ़े गये सपने टुकड़े-टुकड़े होकर धूल-धुसरित हो गये। टूटे सपने तेज धारवाले कांच के टुकड़ों की तरह केवल खून बहाते और पीड़ा बढा़ते हैं। लोगों को लगा कि उस कठोर वास्तविकता से नजर घुमाकर यदि अदूर या सुदूर अतीत की ओर देखा जा सके यदि ऐतिहासिक रोमांस को थोड़ा रंग-रोगन लगाकर लौटाया जा सके तो बुरा क्या है ? इस काल में अनेक शक्तिशाली उपन्याकारों ने इस तरह के उपन्यासों की रचना की। ताराशंकर ने ‘राधा’ और ‘गन्ना’ बेगम’, विभूतिभूषण ने ‘इच्छामती’, प्रमथनाथ बिशी (1901-1965) ने ‘केरी’ साहबेर मुंशी’ एवं विमल मित्र ने ‘बेगम मेरी बिस्वास’ उपन्यास लिखे, तथापि कलकत्ता शहर में एक उपन्यासकार को जिस चैलेंज का सामना करना पड़ता है, उसका सामना वे नहीं कर पाये। ‘हे हृदय मूल फैला दो टूटे पाषाणों में-यह एक वयोवृद्ध का कथन भी है एक उपन्यासकार का अनचाहा संकल्प भी। इसी को लेकर लिखा गया है ताराशंकर का ‘झड़ ओ झरा पाता’ व माणिक बंद्योपाध्याय का ‘चिह्न’ सन् 1946 की कलकत्ता का धधकती पृष्ठभूमि में। किंतु इस अग्निकांड की सारी ज्योति 16 अगस्त के छिन्नमस्तक कलकत्ता के काले वीभत्स धुएं में मलिन पड़ गयी।
बहुत कुछ खोना पड़ा, लेकिन सबसे दुखद और मंहगा पड़ा, सपनों को खोना। इस शताब्दी के पांचवें और छठे दशकों में जिन लोगों ने उपन्यास लिखे उन्होंने मध्यवर्ग की मानसिकता के बीच खडे़ होकर कुछ खोजने का प्रयत्न किया। वे सभी शक्तिशाली गद्य लेखक थे।
नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया द्वारा इस उपन्यास का हिंदी साहित्य ग्यारह भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है।
वे द्वितीय महायुद्ध या उसके तत्काल के बाद के कलकत्ता से परिचित थे। विमल कर का ‘देवाल’ असीम राय का ‘एकालेर कथा’, नरेन्द्रनाथ मित्र का ‘चेनामहल’, संतोषकुमार घोष का ‘किंनु गोलार गली’, ज्योतिरिंद्र नंदी (1917-1975) का ‘बारो घर एक उठान’ आदि सभी उपन्यासों के पात्र यदि विशिष्ट बन पाये हैं तो केवल इस माने में कि इनमें से कोई भी उन्नीसवीं सदी के मध्यवर्ग के पात्रों से मिले उत्तराधिकार की रक्षा के लिए चिंतित नहीं था, होने का कोई कारण भी नहीं था। और इतिहास ने भी अपने नियम के अनुसार उनके हाथों में पकड़ा दी खाली झोली। उसमें जो कुछ पुरानी मुद्राएं थीं भी, उन्हें अब उनके बाजार में भुनाया नहीं जा सकता।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i