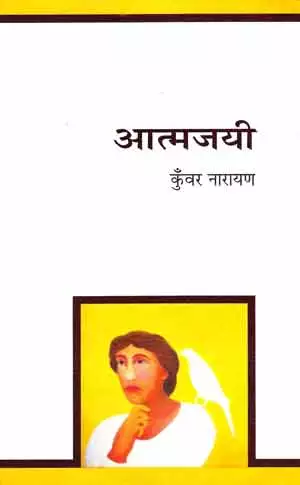|
कविता संग्रह >> आत्मजयी आत्मजयीकुँवर नारायण
|
432 पाठक हैं |
|||||||
मानक प्रबन्ध-काव्य के रूप में प्रशंसित ‘आत्मजयी’ का मूल कथासूत्र कठोपनिषद् में नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
पिछले पच्चीस वर्षों में ‘आत्मजयी’ ने हिन्दी साहित्य
के एक
मानक प्रबन्ध-काव्य के रूप में अपनी एक खास जगह बनायी है और यह अखिल
भारतीय स्तर पर प्रशंसित हुआ है।
‘आत्मजयी’ का मूल कथासूत्र कठोपनिषद् में नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। इस आख्यान के पुराकथात्मक पक्ष को कवि ने आज के मनुष्य की जटिल मनःस्थितियों को एक बेहतर अभिव्यक्ति देने का एक साधन बनाया है।
जीवन के पूर्णानुभव के लिए किसी ऐसे मूल्य के लिए जीना आवश्यक है जो मनुष्य में जीवन की अनश्वरता का बोध कराए। वह सत्य कोई ऐसा जीवन-सत्य हो सकता है जो मरणधर्मा व्यक्तिगत जीवन से बड़ा, अधिक स्थायी या चिरस्थायी हो। यही मनुष्य को सांत्वना दे सकता है कि मर्त्य होते हुए भी वह किसी अमर अर्थ में जी सकता है। जब वह जीवन से केवल कुछ पाने की ही आशा पर चलने वाला असहाय प्राणी नहीं, जीवन को कुछ दे सकने वाला समर्थ मनुष्य होगा तब उसके लिए यह चिन्ता सहसा व्यर्थ हो जाएगी कि जीवन कितना असार है-उसकी मुख्य चिन्ता यह होगी कि वह जीवन को कितना सारपूर्ण बना सकता है।
‘आत्मजयी’ मूलतः मनुष्य की रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनःप्राप्ति की कहानी है। इसमें आधुनिक मनुष्य की जटिल नियति से एक गहरा काव्यात्मक साक्षात्कार है। इतावली भाषा में ‘नचिकेता’ के नाम से इस कृति का अनुवाद प्रकाशित और चर्चित हुआ है-यह इस बात का प्रमाण है कि कवि ने जिन समस्याओं और प्रश्नों से मुठभेड़ की है उनका सार्विक महत्त्व है।
‘आत्मजयी’ का मूल कथासूत्र कठोपनिषद् में नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। इस आख्यान के पुराकथात्मक पक्ष को कवि ने आज के मनुष्य की जटिल मनःस्थितियों को एक बेहतर अभिव्यक्ति देने का एक साधन बनाया है।
जीवन के पूर्णानुभव के लिए किसी ऐसे मूल्य के लिए जीना आवश्यक है जो मनुष्य में जीवन की अनश्वरता का बोध कराए। वह सत्य कोई ऐसा जीवन-सत्य हो सकता है जो मरणधर्मा व्यक्तिगत जीवन से बड़ा, अधिक स्थायी या चिरस्थायी हो। यही मनुष्य को सांत्वना दे सकता है कि मर्त्य होते हुए भी वह किसी अमर अर्थ में जी सकता है। जब वह जीवन से केवल कुछ पाने की ही आशा पर चलने वाला असहाय प्राणी नहीं, जीवन को कुछ दे सकने वाला समर्थ मनुष्य होगा तब उसके लिए यह चिन्ता सहसा व्यर्थ हो जाएगी कि जीवन कितना असार है-उसकी मुख्य चिन्ता यह होगी कि वह जीवन को कितना सारपूर्ण बना सकता है।
‘आत्मजयी’ मूलतः मनुष्य की रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनःप्राप्ति की कहानी है। इसमें आधुनिक मनुष्य की जटिल नियति से एक गहरा काव्यात्मक साक्षात्कार है। इतावली भाषा में ‘नचिकेता’ के नाम से इस कृति का अनुवाद प्रकाशित और चर्चित हुआ है-यह इस बात का प्रमाण है कि कवि ने जिन समस्याओं और प्रश्नों से मुठभेड़ की है उनका सार्विक महत्त्व है।
भूमिका
‘आत्मजयी’ में उठायी गयी समस्या मुख्यतः एक विचारशील
व्यक्ति
की समस्या है। कथानक का नायक नचिकेता मात्र सुखों को अस्वीकार करता है,
तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति-भर ही उसके लिए पर्याप्त नहीं। उसके अन्दर
वह बृहत्तर जिज्ञासा है जिसके लिए केवल सुखी जीना काफ़ी नहीं, सार्थक जीना
ज़रूरी है। यह जिज्ञासा ही उसे उन मनुष्यों की कोटि में रखती है जिन्होंने
सत्य की खोज में अपने हित को गौण माना, और ऐन्द्रिय सुखों के आधार पर ही
जीवन से समझौता नहीं किया, बल्कि उस चरम लक्ष्य के लिए अपना जीवन अर्पित
कर दिया जो उन्हें पाने के योग्य लगा।
नचिकेता की चिन्ता भी अमर जीवन की चिन्ता है। ‘अमर जीवन’ से तात्पर्य उन अमर जीवन-मूल्यों से है जो व्यक्ति-जगत् का अतिक्रमण करके सार्वकालिक और सार्वजनिक बन जाते हैं। नचिकेता इस असाधारण खोज के परिणामों के लिए तैयार है। वह अपने आपको इस धोखे में नहीं रखता कि सत्य से उसे सामान्य अर्थों में सुख ही मिलेगा, लेकिन उसके बिना उसे किसी भी अर्थ में सन्तोष मिल सकेगा, इस बारे में उसे घातक सन्देह है। यम से-साक्षात् मृत्यु तक से-उसका हठ एक दृढ़ जिज्ञासु का हठ है जिसे कोई भी सांसारिक वरदान डिगा नहीं सकता।
नचिकेता अपना सारा जीवन यम या काल, या समय को सौंप देता है। दूसरे शब्दों में वह अपनी चेतना को काय-सापेक्ष समय से मुक्त कर लेता है : वह विशुद्ध ‘अस्तिबोध’ रह जाता है जिसे ‘आत्मा’ कहा जा सकता है। आत्मा का अनुभव तथा इन्द्रियों द्वारा अनुभव, दो अलग बातें मानी गयी हैं। भारत के प्राचीन चिन्तकों ने यदि इन्द्रियों को प्रधानता नहीं दी, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने शरीर या संसार को झूठ माना; बल्कि यह कि उन्होंने बुद्धि और बुद्धि से भी अधिक जो सूक्ष्म हो उस आत्मा को अधिक महत्व दिया। वे कठिन आत्म निग्रह द्वारा सिद्ध करते रहे कि विषयों के अधीन बुद्धि नहीं, बुद्धि के अधीन विषय हैं। शारीरिक जीवन जीते हुए भी शरीर के प्रति अनाशक्त रहा जा सकता है। उनका अनुभव था कि बिना आत्मबल से मनुष्य अपनी शक्तियों का उचित उपयोग नहीं कर सकता, चालक-विहीन रथ की तरह वह निरंकुश अश्वों द्वारा नष्ट-भ्रष्ट कर दिया जायेगा।
किसी भी महान लक्ष्य के लिए अर्पित होने से पहले अपने इस आत्म-विश्वास को पाना अत्यन्त आवश्यक है। तभी मनुष्य अपने लिए, तथा सबके लिए, निजी सुख-सुविधाओं से बृहत्तर कुछ प्राप्त कर सकता है—अपना जीवन किसी अमर अर्थ में जी सकता है। तब वह जीवन से केवल कुछ पाने की ही आशा पर चलने वाला असहाय नहीं, जीवन को कुछ दे सकने वाला समर्थ मनुष्य होगा। उसके लिए तब यह चिन्ता सहसा व्यर्थ हो जायेगी कि जीवन कितना असार है : उसकी मुख्य चिन्ता यह होगी कि वह जीवन को कितना सरसपूर्ण बना सकता है। यथार्थ अब उसके बाहर नहीं, उसमें है, उससे है—अन्यथा वह कुछ नहीं है। सम्पूर्ण बाह्य परिस्थितियों या तो उसकी चेतना से विकीर्ण है—चेतना जो उसके वश में है, चीजों के वश में नहीं—या फिर अंधेरी है। वह चाहे तो सब कुछ अस्वीकार करके स्वयं को काल से लौटा दे : चाहे तो उसे स्वीकार करके एक नया अर्थ दें।
पहली परिस्थिति में नचिकेता अपने आपको काल को सौंप देता है अर्थात् वह दिये हुए बाह्य जीवन को अस्वीकार करता है। आन्तरिक जीवन के प्रति सचेत होते हुए भी वह अभी अपने में उस आत्म-शक्ति का विकास नहीं कर पाया है जो बाहरी परिस्थितियों से विचलित न हो। वह निराशा के उस चरम बिन्दु पर पहुँच जाता है जहाँ साधारण जीवन कोई सान्त्वना नहीं। अस्तित्व पूर्णतः निरर्थक और असार लगता है। मन की वह वीतराग दशा जब सारे भौतिक मूल्य समाप्त हो जाते हैं-अस्तित्व जगत्-सापेक्ष नहीं रह जाता। स्वयं को सोचता हुआ व्यक्ति ही एक इकाई रह जाता है जिसके सामने दूसरी इकाई है केवल एक अनिर्वच महाशून्य वह है और उसके चारों ओर एक सपाट अँधेरा, उस अँधेरे में ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें वह अपनी चेतना को लिप्त रख सके। आत्महत्या ही उसे एक रास्ता दिखाई देता है। भय-मिश्रित उत्कण्ठा उसके समस्त जीवन-बोध को आक्रान्त कर लेती है।
पास्काल का कहना है कि इस अनन्त विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। ‘यह गुम्बदे मीनाई, यह आलमें तनहाई। मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई।’ में इक़बाल का संकेत भी उसी ‘भय’ की ओर है जिसे हम जगह-जगह साहित्य और दर्शन में व्यक्त पाते हैं और जो आधुनिक अस्तित्ववादी दर्शन के भी मूल आधारों में से है। लेकिन इस ‘भय’ या ‘उत्कण्ठा’ का परिणाम अन्ततः निराशावादी ही होगा, ऐसा मानना भारतीय के एक महत्त्वपूर्ण स्थिति-निरूपण को ही गलत समझना होगा। मृत्यु के चिन्तन से जीवन के प्रति निराशा ही पैदा हो, ऐसा आवश्यक नहीं है—कोई नितान्त मौलिक दृष्टिकोण भी जन्म पा सकता है। मृत्यु की गहरी अनुभूति ने जीवन को असमर्थ कर दिया हो, इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ चिन्तक की दृष्टि कुछ इस तरह पैनी हुई कि वह मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली कुछ दे जाने के प्रयत्न में कोई असाधारण निधि दे गया।
बृहदारण्य में ‘अभयं वै ब्रह्म’ में विश्वास करने वाले याज्ञवल्क्य ज्ञान के जिस आदर्श को प्रतिष्ठित कर गये वह मृत्यु के परे की चीज़ है। बुद्ध भी रोग, जरा, मृत्यु को विचारते हुए जीवन को एक ऐसा दर्शन दे गये जो उनके बाद सैकड़ों वर्षों से जीवित है। शंकराचार्य, कबीर आदि अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनकी सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि मृत्यु की तीव्र अनुभूति के कारण उत्तेजित हुई। मृत्यु के प्रति निरपेक्ष भी रहा जा सकता है, जैसे जीवन के बहुत-से तथ्यों के प्रति निरपेक्ष रहते हुए कामचलाऊ जीवन-दर्शन बना लिया जा सकता है। लेकिन मैं इस भय को निरादार मानता हूँ कि मृत्यु का चिन्तन भी जीवन के लिए उसी प्रकार घातक होगा जैसे मृत्यु स्वयं ! मृत्यु को सोचने का यही परिणाम नहीं है कि आदमी उसके सामने घुटने टेक दे और हताश होकर बैठा रहे। वह ऐसा कुछ करना चाह सकता है जिसे मृत्यु कभी, या आसानी से, नष्ट न कर सके। मृत्यु का सामना करना, उस पर विजयी होने की कामना भी बिलकुल स्वाभाविक है। मृत्यु से बड़ा होने के प्रयत्न में वह जीवन से ही बड़ा हो सकता है। लेकिन यदि हम जीवन से मृत्यु के बारे में सोचना ही निकाल दें, तो अधिक सम्भावना यही है कि हम किसी ऐसे जीवन दर्शन को अपनाकर चलेंगे जिसकी तत्कालिक सफलता उतनी ही आसान है और कल्पना रहित होगी जितनी वह अस्थायी होगी। अगर हम उतने ही से सन्तुष्ट हो सकते हैं जितने से मृत्यु के बारे में कभी न सोचने वाले प्राणी हुआ करते हैं, तो मृत्यु क्या किसी भी यथार्थ के बारे में गम्भीर चिन्तन की दलील व्यर्थ हैं।
यह आत्महत्या का बिन्दु, जिस पर नचिकेता पहुँचता है, मुझे अत्यन्त महत्वपूर्ण लगा-प्राचीन तथा आधुनिक दोनों ही सन्दर्भों में। भारतीय दर्शन की तो शायद ही ऐसी कोई महत्वपूर्ण धारा हो जिसका प्रवर्तक इस तरह की वीतराग स्थिति से नहीं गुजरता। मृत्यु को विचारते हुए सहसा भिन्न नहीं। इसी प्रकार गीता में, ‘युद्ध नहीं करूँगा’ कहकर अर्जुन जब हथियार डाल देता है उस समय जीवन की असारता के प्रति नचिकेता की ही तरह वे सब भी अपने आपको किसी न किसी रूप में संसार की अपेक्षा समाप्त कर लेते हैं।
हम देखते हैं कि इस बिन्दु से प्रत्येक चिन्तक लौटता है—फिर एक बार जीवन की ओर। वह फिर से जीवन को जीता है किसी ऐसे सत्य के लिए जिसे वह समझता है अमर है। यही उसका शाश्वत जीवन है, अमर जीवन है। वह सत्य ‘निर्वाण’ हो सकता है, वह सत्य ‘ईश्वर’ हो सकता है, वह सत्य ‘ब्रह्म’ हो सकता है—वह सत्य कोई ऐसा जीवन सत्य हो सकता है जो मरणधर्मा व्यक्तिगत जीवन से बड़ा हो, अधिक स्थाई हो, या चिर स्थाई हो।
वे इस सार्थक अनुभूति तक पहुँचते हैं कि निजी सुख-सुविधा की खोज ही जीवन का चरम लक्ष्य नहीं। उससे कोई स्थायी सन्तोष—और एक विचारशील मनुष्य के लिए अस्थायी सन्तोष तक—मिलना कठिन है। जीवन के पूर्वानुभव के लिए किसी ऐसे मूल्य के लिए जीना आवश्यक है जो जीवन की अनश्वरता का बोध कराये। यही मनुष्य को सान्त्वना दे सका है कि मर्त्य होते हुए भी वह किसी अमर अर्थ में जी सकता है।
‘आत्मजयी’ में मैंने केवल इस दृष्टिकोण भर को सामने रखने का प्रयत्न किया है—किसी निश्चित दार्शनिक या नैतिक या धार्मिक या सामाजिक मूल्य का प्रतिपादन नहीं। ‘‘आत्मजयी’ मूलतः जीवन की सृजनात्मक सम्भावनाओं में आस्था के पुनर्लाभ की कहानी है।
‘कठोपनिषद्’ से लिये गये नचिकेता के कथानक में मैंने थोड़ा परिवर्तन किया है, लेकिन इतना नहीं कि आधार-कथा की वस्तु-स्थितियाँ ही भिन्न हो गयी हों। कथा को आधुनिक ढंग से देखा गया है, पौराणिक दिव्य-कथा के रूप में नहीं।
अपने पिता वाजश्रवा से धर्म-कर्म सम्बन्धी मतभेदों के परिणाम-स्वरूप अत्यन्त खिन्न नचिकेता आत्महत्या के लिए अपने को पानी में डुबा देता है। मेरे द्वारा लिये गए प्रसंग में यह अपेक्षित है कि वह वास्तव में मरता नहीं, मरने से पहले ही पानी से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन अचेतावस्था में वह स्वप्न देखता है—यम से साक्षात्कार। यम उसके अन्तर्मन में स्थित मृत्यु का ही पौराणिक रूप है। कठोपनिषद् में उसे तीन दिन तक यम के द्वार पर भूखा-प्यासा यम के लौटने की प्रतीक्षा करते दिखाया गया है। लौटने पर यम अतिथि के प्रति हो गयी इस अप्रत्याशित उपेक्षा के प्रतिकार-स्वरूप उसे तीन वरदान देते हैं।
पहला यह कि वाजश्रवा का नचिकेता के प्रति क्रोध शान्त हो, दूसरा यज्ञों की नचिकेताग्नि, तीसरा मृत्यु के रहस्य का उद्घाटन। मैंने ‘आत्मजयी’ से पहले और तीसरे वरदान के आधार पर ही जीवन-सम्बन्धी कुछ धारणाओं पर विचार किया है।
नचिकेता और वाजश्रवा की सहमति, तथा वाजश्रवा का क्रोध में नचिकेता को मृत्यु दे देना, न केवल नयी और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष का प्रतीक है बल्कि उन वस्तु परक वैदिक तथा आत्मपरक उपनिष्त्कालीन दृष्टिकोण का भी प्रतीक है जिनका एक रूप हम आज के अपने जीवन में भी पाते हैं। एक ओर तो हमारी भयावह भौतिक उन्नति, दूसरी ओर आत्मिक स्तर पर वह घोर असंयम जो इस भौतिक प्रगति को अपने लिए अभिशाप बनाये ले रहा है। वैदिककालीन मनुष्य भी आज की ही तरह, यद्यपि आज से कहीं अधिक सीमित परिवेश में, प्राकृतिक शक्तियों को यज्ञादि द्वारा अपने अनुकूल रखना चाहता था। उसका दृष्टिकोण मूलतः वस्तुवादी था जिसकी प्रतिक्रिया में ही उपनिष्त्कालीन अध्यात्म का विकास हुआ।
परोक्ष रूप से मेरे मन में यह साम्य भी था कि वाजश्रवा वैदिककालीन वस्तुवादी दृष्टिकोण का प्रतीक है और नचिकेता उपनिष्तकालीन आत्म-पक्ष का। उपनिषद् आत्मा या मनुष्य के आन्तरिक जीवन को प्राथमिकता देते हैं, यह मानते हुए कि बिना जीवन को आन्तरिक स्तर पर संयमित किये सारी भौतिक प्रगति न केवल बेकार बल्कि ख़तरनाक साबित हो सकती है। स्पष्टतः नचिकेता पर यह तर्क लागू नहीं होता कि यदि एक व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक जीवन सन्तुष्ट है, तो उसका आन्तरिक जीवन भी सन्तुष्ट होगा। सच पूछा जाये तो नचिकेता के सारे असन्तोष और विद्रोह का मूल कारण ही वह वस्तुवादी दृष्टिकोण है जो मृत्यु के आगे उसे कोई सान्त्वना नहीं दे पाता। नचिकेता जीवन के प्रति असम्मान नहीं दिखाता, क्योंकि उसके स्वभाव में कुण्ठा या विकृति नहीं है। बाद में उसके जीवन को फिर से स्वीकार करना, इस बात का द्योतक है कि उसका विरोध जीवन से नहीं, उस दृष्टिकोण से है जो जीवन को सीमित कर दे।
‘मृत्युमुखात्प्रमुक्तम्’ खण्ड होश में आये नचिकेता की वे प्रक्रियाएँ हैं जब वह अपने जीवन को एक तरह से पूरा खो चुकने के बाद फिर से प्राप्त करता है, और यह अद्वितीय उपलब्धि है उसे नये सिरे से जीने के एक महान् अवसर का बोध कराती है। जीवन को इस तरह खोकर ही वह उसके वास्तविक मूल्य का अनुभव कर पाता है। यही वह दूसरी परिस्थित है जब एक चिन्तक एक बार जीवन से उपराम होकर आत्महत्या के बिन्दु से पुनः जीवन की ओर लौटता है। गीता के शब्दों में, आसक्त भाव से नहीं—आत्म-शक्ति को पूर्णतः प्राप्त करके।
ये कविताएँ ‘कठोपनिषद्’ की व्याख्या नहीं है। ‘कठोपनिषद्’ के विभिन्न श्लोकों से केवल संकेत-भर ही लिया गया है-बिना उनके अर्थ या कठोपनिषद् में उनके क्रम को, कविताओं के लिए किसी प्रकार का बन्धन माने। अकसर कविताओं और श्लोकों के मन्तव्यों में बुनियादी अन्तर तक मिल सकता है, लेकिन इस अन्तर के बावजूद प्रयत्न यही रहा है कि सम्पूर्ण कृति में वैचारिक विषमता न आने पाये।
‘आत्मजयी’ में ली गयी समस्या नयी नहीं-उतनी ही पुरानी है (या फिर उतनी ही नयी) जितना जीवन और मृत्यु सम्बन्धी मनुष्य का अनुभव। इस अनुभव को पौराणिक सन्दर्भ में रखते समय यह चिन्ता बराबर रही कि कहीं हिन्दी की रूढ़ आध्यात्मिक शब्दावली अनुभव की सचाई पर इस तरह न हावी हो जाये कि ‘आत्मजयी’ को एक आधुनिक कृति के रूप में पहचानना ही कठिन हो। उपनिषद् यम, नचिकेता, आत्मा, मृत्यु, ब्रह्म...किसी भी नये कवि के लिए इन प्राचीन शब्दों की अश्वत्थ जड़ें, प्रेरणा शायद कम, चेतावनी अधिक होनी चाहिए। फिर भी मैंने यदि इस बीहड़ वन में प्रवेश करने का दुस्साहस किया, तो उसका एक कारण यह भी था कि मुझे ये शब्द वास्तव में उतने बीहड़ नहीं लगे जितने उन्हें ठीक से न समझने वाले व्याख्याकारों ने बना रखा है। उन्हें आधुनिक व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं के सन्दर्भ में भी जाँचा जा सकता है। ऐसी आशा ने भी इस ओर प्रेरित किया।
यूनानी पुरा कथाओं की ही तरह भारतीय पुराकथाएँ भी आरम्भ में रहस्यवादी ढंग की नहीं थीं, मनुष्य और प्रकृति के बीच बड़े ही घनिष्ठ सम्बन्धों का रोचक और जीवन्त कथा—रूप थीं। लेकिन आज हिन्दू धर्म और हिन्दू पौराणिक अतीत को अलग कर सकना लगभग असम्भव है; जबकि ग्रीक पुराकथाएँ ईसाई धर्म और यूरोपीय रहस्यवाद से लगभग अछूती रहीं। भारतीय पुराकथाओं पर परिवर्ती धार्मिक रंग इतना गहरा है कि उसे विशुद्ध मानवीय महत्त्व दे सकना कठिन लगता है। ग्रीक पुराकथाओं में आदि-मानव की अन्तः प्रकृति का अधिक अरंजित रूप सुरक्षित मिलता है। इसीलिए कामू का ‘सिसीफ़स’ या जेम्स जॉयस का ‘यूलिसिस’ पुराकथात्मक चरित्र होते हुए भी धार्मिक चरित्र नहीं लगते—उन्हें ‘साहस’ जैसे नितान्त मानवीय गुण का प्रतीक मानकर चलने में उस प्रकार का धार्मिक व्यवधान बीच में नहीं आता, जैसा अवतारवाद के कारण भारतीय देवी-देवताओं के साथ आता है।
नचिकेता का प्रसंग इस दृष्टि से मुझे विशेष उपयुक्त लगा कि वह मुख्यतः धार्मिक क्षेत्र का न होकर दार्शनिक क्षेत्र का ही रहा, जहाँ वैचारिक स्वतन्त्रता के लिए अधिक गुंजाइश है। दूसरे, नचिकेता के बाद में जो थोड़ा-बहुत साहित्य लिखा भी गया है उसकी ऐसी साश्वत परम्परा नहीं जो उसे फिर कोई नया साहित्यिक रूप देने में बाधक हो—न अब तक इस आख्यान के पुराकथात्मक पक्ष को ही इस प्रकार लिया गया है कि वह आज के मनुष्य की जटिल मनःस्थितियों को बेहतर अभिव्यक्ति दे सके। इसीलिए मैंने ‘आत्मजयी’ के धार्मिक या दाशर्निक पक्ष की विशेष चिन्ता न करके उन मानवीय अनुभवों पर अधिक दबाव डाला है जिनसे आज का मनुष्य भी गुज़र रहा है, और जिनका नचिकेता मुझे एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक लगा।
‘आत्मजयी’ एक बार में नहीं लिखा गया है, थोड़ा बहुत काम अरसे से चलता रहा है। इस बीच इसमें काफी परिवर्तन हुए और ‘आत्मजयी’ अब जिस रूप में पाठकों के सामने है उसके पीछे कई योग्य मित्रों के समय-समय पर मिलते रहे अमूल्य सुझाव और स्नेहपूर्ण सम्मतियाँ भी हैं। मैं उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ।
नचिकेता की चिन्ता भी अमर जीवन की चिन्ता है। ‘अमर जीवन’ से तात्पर्य उन अमर जीवन-मूल्यों से है जो व्यक्ति-जगत् का अतिक्रमण करके सार्वकालिक और सार्वजनिक बन जाते हैं। नचिकेता इस असाधारण खोज के परिणामों के लिए तैयार है। वह अपने आपको इस धोखे में नहीं रखता कि सत्य से उसे सामान्य अर्थों में सुख ही मिलेगा, लेकिन उसके बिना उसे किसी भी अर्थ में सन्तोष मिल सकेगा, इस बारे में उसे घातक सन्देह है। यम से-साक्षात् मृत्यु तक से-उसका हठ एक दृढ़ जिज्ञासु का हठ है जिसे कोई भी सांसारिक वरदान डिगा नहीं सकता।
नचिकेता अपना सारा जीवन यम या काल, या समय को सौंप देता है। दूसरे शब्दों में वह अपनी चेतना को काय-सापेक्ष समय से मुक्त कर लेता है : वह विशुद्ध ‘अस्तिबोध’ रह जाता है जिसे ‘आत्मा’ कहा जा सकता है। आत्मा का अनुभव तथा इन्द्रियों द्वारा अनुभव, दो अलग बातें मानी गयी हैं। भारत के प्राचीन चिन्तकों ने यदि इन्द्रियों को प्रधानता नहीं दी, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने शरीर या संसार को झूठ माना; बल्कि यह कि उन्होंने बुद्धि और बुद्धि से भी अधिक जो सूक्ष्म हो उस आत्मा को अधिक महत्व दिया। वे कठिन आत्म निग्रह द्वारा सिद्ध करते रहे कि विषयों के अधीन बुद्धि नहीं, बुद्धि के अधीन विषय हैं। शारीरिक जीवन जीते हुए भी शरीर के प्रति अनाशक्त रहा जा सकता है। उनका अनुभव था कि बिना आत्मबल से मनुष्य अपनी शक्तियों का उचित उपयोग नहीं कर सकता, चालक-विहीन रथ की तरह वह निरंकुश अश्वों द्वारा नष्ट-भ्रष्ट कर दिया जायेगा।
किसी भी महान लक्ष्य के लिए अर्पित होने से पहले अपने इस आत्म-विश्वास को पाना अत्यन्त आवश्यक है। तभी मनुष्य अपने लिए, तथा सबके लिए, निजी सुख-सुविधाओं से बृहत्तर कुछ प्राप्त कर सकता है—अपना जीवन किसी अमर अर्थ में जी सकता है। तब वह जीवन से केवल कुछ पाने की ही आशा पर चलने वाला असहाय नहीं, जीवन को कुछ दे सकने वाला समर्थ मनुष्य होगा। उसके लिए तब यह चिन्ता सहसा व्यर्थ हो जायेगी कि जीवन कितना असार है : उसकी मुख्य चिन्ता यह होगी कि वह जीवन को कितना सरसपूर्ण बना सकता है। यथार्थ अब उसके बाहर नहीं, उसमें है, उससे है—अन्यथा वह कुछ नहीं है। सम्पूर्ण बाह्य परिस्थितियों या तो उसकी चेतना से विकीर्ण है—चेतना जो उसके वश में है, चीजों के वश में नहीं—या फिर अंधेरी है। वह चाहे तो सब कुछ अस्वीकार करके स्वयं को काल से लौटा दे : चाहे तो उसे स्वीकार करके एक नया अर्थ दें।
पहली परिस्थिति में नचिकेता अपने आपको काल को सौंप देता है अर्थात् वह दिये हुए बाह्य जीवन को अस्वीकार करता है। आन्तरिक जीवन के प्रति सचेत होते हुए भी वह अभी अपने में उस आत्म-शक्ति का विकास नहीं कर पाया है जो बाहरी परिस्थितियों से विचलित न हो। वह निराशा के उस चरम बिन्दु पर पहुँच जाता है जहाँ साधारण जीवन कोई सान्त्वना नहीं। अस्तित्व पूर्णतः निरर्थक और असार लगता है। मन की वह वीतराग दशा जब सारे भौतिक मूल्य समाप्त हो जाते हैं-अस्तित्व जगत्-सापेक्ष नहीं रह जाता। स्वयं को सोचता हुआ व्यक्ति ही एक इकाई रह जाता है जिसके सामने दूसरी इकाई है केवल एक अनिर्वच महाशून्य वह है और उसके चारों ओर एक सपाट अँधेरा, उस अँधेरे में ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें वह अपनी चेतना को लिप्त रख सके। आत्महत्या ही उसे एक रास्ता दिखाई देता है। भय-मिश्रित उत्कण्ठा उसके समस्त जीवन-बोध को आक्रान्त कर लेती है।
पास्काल का कहना है कि इस अनन्त विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। ‘यह गुम्बदे मीनाई, यह आलमें तनहाई। मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई।’ में इक़बाल का संकेत भी उसी ‘भय’ की ओर है जिसे हम जगह-जगह साहित्य और दर्शन में व्यक्त पाते हैं और जो आधुनिक अस्तित्ववादी दर्शन के भी मूल आधारों में से है। लेकिन इस ‘भय’ या ‘उत्कण्ठा’ का परिणाम अन्ततः निराशावादी ही होगा, ऐसा मानना भारतीय के एक महत्त्वपूर्ण स्थिति-निरूपण को ही गलत समझना होगा। मृत्यु के चिन्तन से जीवन के प्रति निराशा ही पैदा हो, ऐसा आवश्यक नहीं है—कोई नितान्त मौलिक दृष्टिकोण भी जन्म पा सकता है। मृत्यु की गहरी अनुभूति ने जीवन को असमर्थ कर दिया हो, इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ चिन्तक की दृष्टि कुछ इस तरह पैनी हुई कि वह मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली कुछ दे जाने के प्रयत्न में कोई असाधारण निधि दे गया।
बृहदारण्य में ‘अभयं वै ब्रह्म’ में विश्वास करने वाले याज्ञवल्क्य ज्ञान के जिस आदर्श को प्रतिष्ठित कर गये वह मृत्यु के परे की चीज़ है। बुद्ध भी रोग, जरा, मृत्यु को विचारते हुए जीवन को एक ऐसा दर्शन दे गये जो उनके बाद सैकड़ों वर्षों से जीवित है। शंकराचार्य, कबीर आदि अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनकी सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि मृत्यु की तीव्र अनुभूति के कारण उत्तेजित हुई। मृत्यु के प्रति निरपेक्ष भी रहा जा सकता है, जैसे जीवन के बहुत-से तथ्यों के प्रति निरपेक्ष रहते हुए कामचलाऊ जीवन-दर्शन बना लिया जा सकता है। लेकिन मैं इस भय को निरादार मानता हूँ कि मृत्यु का चिन्तन भी जीवन के लिए उसी प्रकार घातक होगा जैसे मृत्यु स्वयं ! मृत्यु को सोचने का यही परिणाम नहीं है कि आदमी उसके सामने घुटने टेक दे और हताश होकर बैठा रहे। वह ऐसा कुछ करना चाह सकता है जिसे मृत्यु कभी, या आसानी से, नष्ट न कर सके। मृत्यु का सामना करना, उस पर विजयी होने की कामना भी बिलकुल स्वाभाविक है। मृत्यु से बड़ा होने के प्रयत्न में वह जीवन से ही बड़ा हो सकता है। लेकिन यदि हम जीवन से मृत्यु के बारे में सोचना ही निकाल दें, तो अधिक सम्भावना यही है कि हम किसी ऐसे जीवन दर्शन को अपनाकर चलेंगे जिसकी तत्कालिक सफलता उतनी ही आसान है और कल्पना रहित होगी जितनी वह अस्थायी होगी। अगर हम उतने ही से सन्तुष्ट हो सकते हैं जितने से मृत्यु के बारे में कभी न सोचने वाले प्राणी हुआ करते हैं, तो मृत्यु क्या किसी भी यथार्थ के बारे में गम्भीर चिन्तन की दलील व्यर्थ हैं।
यह आत्महत्या का बिन्दु, जिस पर नचिकेता पहुँचता है, मुझे अत्यन्त महत्वपूर्ण लगा-प्राचीन तथा आधुनिक दोनों ही सन्दर्भों में। भारतीय दर्शन की तो शायद ही ऐसी कोई महत्वपूर्ण धारा हो जिसका प्रवर्तक इस तरह की वीतराग स्थिति से नहीं गुजरता। मृत्यु को विचारते हुए सहसा भिन्न नहीं। इसी प्रकार गीता में, ‘युद्ध नहीं करूँगा’ कहकर अर्जुन जब हथियार डाल देता है उस समय जीवन की असारता के प्रति नचिकेता की ही तरह वे सब भी अपने आपको किसी न किसी रूप में संसार की अपेक्षा समाप्त कर लेते हैं।
हम देखते हैं कि इस बिन्दु से प्रत्येक चिन्तक लौटता है—फिर एक बार जीवन की ओर। वह फिर से जीवन को जीता है किसी ऐसे सत्य के लिए जिसे वह समझता है अमर है। यही उसका शाश्वत जीवन है, अमर जीवन है। वह सत्य ‘निर्वाण’ हो सकता है, वह सत्य ‘ईश्वर’ हो सकता है, वह सत्य ‘ब्रह्म’ हो सकता है—वह सत्य कोई ऐसा जीवन सत्य हो सकता है जो मरणधर्मा व्यक्तिगत जीवन से बड़ा हो, अधिक स्थाई हो, या चिर स्थाई हो।
वे इस सार्थक अनुभूति तक पहुँचते हैं कि निजी सुख-सुविधा की खोज ही जीवन का चरम लक्ष्य नहीं। उससे कोई स्थायी सन्तोष—और एक विचारशील मनुष्य के लिए अस्थायी सन्तोष तक—मिलना कठिन है। जीवन के पूर्वानुभव के लिए किसी ऐसे मूल्य के लिए जीना आवश्यक है जो जीवन की अनश्वरता का बोध कराये। यही मनुष्य को सान्त्वना दे सका है कि मर्त्य होते हुए भी वह किसी अमर अर्थ में जी सकता है।
‘आत्मजयी’ में मैंने केवल इस दृष्टिकोण भर को सामने रखने का प्रयत्न किया है—किसी निश्चित दार्शनिक या नैतिक या धार्मिक या सामाजिक मूल्य का प्रतिपादन नहीं। ‘‘आत्मजयी’ मूलतः जीवन की सृजनात्मक सम्भावनाओं में आस्था के पुनर्लाभ की कहानी है।
‘कठोपनिषद्’ से लिये गये नचिकेता के कथानक में मैंने थोड़ा परिवर्तन किया है, लेकिन इतना नहीं कि आधार-कथा की वस्तु-स्थितियाँ ही भिन्न हो गयी हों। कथा को आधुनिक ढंग से देखा गया है, पौराणिक दिव्य-कथा के रूप में नहीं।
अपने पिता वाजश्रवा से धर्म-कर्म सम्बन्धी मतभेदों के परिणाम-स्वरूप अत्यन्त खिन्न नचिकेता आत्महत्या के लिए अपने को पानी में डुबा देता है। मेरे द्वारा लिये गए प्रसंग में यह अपेक्षित है कि वह वास्तव में मरता नहीं, मरने से पहले ही पानी से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन अचेतावस्था में वह स्वप्न देखता है—यम से साक्षात्कार। यम उसके अन्तर्मन में स्थित मृत्यु का ही पौराणिक रूप है। कठोपनिषद् में उसे तीन दिन तक यम के द्वार पर भूखा-प्यासा यम के लौटने की प्रतीक्षा करते दिखाया गया है। लौटने पर यम अतिथि के प्रति हो गयी इस अप्रत्याशित उपेक्षा के प्रतिकार-स्वरूप उसे तीन वरदान देते हैं।
पहला यह कि वाजश्रवा का नचिकेता के प्रति क्रोध शान्त हो, दूसरा यज्ञों की नचिकेताग्नि, तीसरा मृत्यु के रहस्य का उद्घाटन। मैंने ‘आत्मजयी’ से पहले और तीसरे वरदान के आधार पर ही जीवन-सम्बन्धी कुछ धारणाओं पर विचार किया है।
नचिकेता और वाजश्रवा की सहमति, तथा वाजश्रवा का क्रोध में नचिकेता को मृत्यु दे देना, न केवल नयी और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष का प्रतीक है बल्कि उन वस्तु परक वैदिक तथा आत्मपरक उपनिष्त्कालीन दृष्टिकोण का भी प्रतीक है जिनका एक रूप हम आज के अपने जीवन में भी पाते हैं। एक ओर तो हमारी भयावह भौतिक उन्नति, दूसरी ओर आत्मिक स्तर पर वह घोर असंयम जो इस भौतिक प्रगति को अपने लिए अभिशाप बनाये ले रहा है। वैदिककालीन मनुष्य भी आज की ही तरह, यद्यपि आज से कहीं अधिक सीमित परिवेश में, प्राकृतिक शक्तियों को यज्ञादि द्वारा अपने अनुकूल रखना चाहता था। उसका दृष्टिकोण मूलतः वस्तुवादी था जिसकी प्रतिक्रिया में ही उपनिष्त्कालीन अध्यात्म का विकास हुआ।
परोक्ष रूप से मेरे मन में यह साम्य भी था कि वाजश्रवा वैदिककालीन वस्तुवादी दृष्टिकोण का प्रतीक है और नचिकेता उपनिष्तकालीन आत्म-पक्ष का। उपनिषद् आत्मा या मनुष्य के आन्तरिक जीवन को प्राथमिकता देते हैं, यह मानते हुए कि बिना जीवन को आन्तरिक स्तर पर संयमित किये सारी भौतिक प्रगति न केवल बेकार बल्कि ख़तरनाक साबित हो सकती है। स्पष्टतः नचिकेता पर यह तर्क लागू नहीं होता कि यदि एक व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक जीवन सन्तुष्ट है, तो उसका आन्तरिक जीवन भी सन्तुष्ट होगा। सच पूछा जाये तो नचिकेता के सारे असन्तोष और विद्रोह का मूल कारण ही वह वस्तुवादी दृष्टिकोण है जो मृत्यु के आगे उसे कोई सान्त्वना नहीं दे पाता। नचिकेता जीवन के प्रति असम्मान नहीं दिखाता, क्योंकि उसके स्वभाव में कुण्ठा या विकृति नहीं है। बाद में उसके जीवन को फिर से स्वीकार करना, इस बात का द्योतक है कि उसका विरोध जीवन से नहीं, उस दृष्टिकोण से है जो जीवन को सीमित कर दे।
‘मृत्युमुखात्प्रमुक्तम्’ खण्ड होश में आये नचिकेता की वे प्रक्रियाएँ हैं जब वह अपने जीवन को एक तरह से पूरा खो चुकने के बाद फिर से प्राप्त करता है, और यह अद्वितीय उपलब्धि है उसे नये सिरे से जीने के एक महान् अवसर का बोध कराती है। जीवन को इस तरह खोकर ही वह उसके वास्तविक मूल्य का अनुभव कर पाता है। यही वह दूसरी परिस्थित है जब एक चिन्तक एक बार जीवन से उपराम होकर आत्महत्या के बिन्दु से पुनः जीवन की ओर लौटता है। गीता के शब्दों में, आसक्त भाव से नहीं—आत्म-शक्ति को पूर्णतः प्राप्त करके।
ये कविताएँ ‘कठोपनिषद्’ की व्याख्या नहीं है। ‘कठोपनिषद्’ के विभिन्न श्लोकों से केवल संकेत-भर ही लिया गया है-बिना उनके अर्थ या कठोपनिषद् में उनके क्रम को, कविताओं के लिए किसी प्रकार का बन्धन माने। अकसर कविताओं और श्लोकों के मन्तव्यों में बुनियादी अन्तर तक मिल सकता है, लेकिन इस अन्तर के बावजूद प्रयत्न यही रहा है कि सम्पूर्ण कृति में वैचारिक विषमता न आने पाये।
‘आत्मजयी’ में ली गयी समस्या नयी नहीं-उतनी ही पुरानी है (या फिर उतनी ही नयी) जितना जीवन और मृत्यु सम्बन्धी मनुष्य का अनुभव। इस अनुभव को पौराणिक सन्दर्भ में रखते समय यह चिन्ता बराबर रही कि कहीं हिन्दी की रूढ़ आध्यात्मिक शब्दावली अनुभव की सचाई पर इस तरह न हावी हो जाये कि ‘आत्मजयी’ को एक आधुनिक कृति के रूप में पहचानना ही कठिन हो। उपनिषद् यम, नचिकेता, आत्मा, मृत्यु, ब्रह्म...किसी भी नये कवि के लिए इन प्राचीन शब्दों की अश्वत्थ जड़ें, प्रेरणा शायद कम, चेतावनी अधिक होनी चाहिए। फिर भी मैंने यदि इस बीहड़ वन में प्रवेश करने का दुस्साहस किया, तो उसका एक कारण यह भी था कि मुझे ये शब्द वास्तव में उतने बीहड़ नहीं लगे जितने उन्हें ठीक से न समझने वाले व्याख्याकारों ने बना रखा है। उन्हें आधुनिक व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं के सन्दर्भ में भी जाँचा जा सकता है। ऐसी आशा ने भी इस ओर प्रेरित किया।
यूनानी पुरा कथाओं की ही तरह भारतीय पुराकथाएँ भी आरम्भ में रहस्यवादी ढंग की नहीं थीं, मनुष्य और प्रकृति के बीच बड़े ही घनिष्ठ सम्बन्धों का रोचक और जीवन्त कथा—रूप थीं। लेकिन आज हिन्दू धर्म और हिन्दू पौराणिक अतीत को अलग कर सकना लगभग असम्भव है; जबकि ग्रीक पुराकथाएँ ईसाई धर्म और यूरोपीय रहस्यवाद से लगभग अछूती रहीं। भारतीय पुराकथाओं पर परिवर्ती धार्मिक रंग इतना गहरा है कि उसे विशुद्ध मानवीय महत्त्व दे सकना कठिन लगता है। ग्रीक पुराकथाओं में आदि-मानव की अन्तः प्रकृति का अधिक अरंजित रूप सुरक्षित मिलता है। इसीलिए कामू का ‘सिसीफ़स’ या जेम्स जॉयस का ‘यूलिसिस’ पुराकथात्मक चरित्र होते हुए भी धार्मिक चरित्र नहीं लगते—उन्हें ‘साहस’ जैसे नितान्त मानवीय गुण का प्रतीक मानकर चलने में उस प्रकार का धार्मिक व्यवधान बीच में नहीं आता, जैसा अवतारवाद के कारण भारतीय देवी-देवताओं के साथ आता है।
नचिकेता का प्रसंग इस दृष्टि से मुझे विशेष उपयुक्त लगा कि वह मुख्यतः धार्मिक क्षेत्र का न होकर दार्शनिक क्षेत्र का ही रहा, जहाँ वैचारिक स्वतन्त्रता के लिए अधिक गुंजाइश है। दूसरे, नचिकेता के बाद में जो थोड़ा-बहुत साहित्य लिखा भी गया है उसकी ऐसी साश्वत परम्परा नहीं जो उसे फिर कोई नया साहित्यिक रूप देने में बाधक हो—न अब तक इस आख्यान के पुराकथात्मक पक्ष को ही इस प्रकार लिया गया है कि वह आज के मनुष्य की जटिल मनःस्थितियों को बेहतर अभिव्यक्ति दे सके। इसीलिए मैंने ‘आत्मजयी’ के धार्मिक या दाशर्निक पक्ष की विशेष चिन्ता न करके उन मानवीय अनुभवों पर अधिक दबाव डाला है जिनसे आज का मनुष्य भी गुज़र रहा है, और जिनका नचिकेता मुझे एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक लगा।
‘आत्मजयी’ एक बार में नहीं लिखा गया है, थोड़ा बहुत काम अरसे से चलता रहा है। इस बीच इसमें काफी परिवर्तन हुए और ‘आत्मजयी’ अब जिस रूप में पाठकों के सामने है उसके पीछे कई योग्य मित्रों के समय-समय पर मिलते रहे अमूल्य सुझाव और स्नेहपूर्ण सम्मतियाँ भी हैं। मैं उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ।
पूर्वाभास
ओ मस्तक विराट,
अभी नहीं मुकुट और अलंकार।
अभी नहीं तिलक और राज्यभार।
तेजस्वी चिन्तित ललाट। दो मुझको
सदियों तपस्याओं में जी सकने की क्षमता।
पाऊँ कदाचित् वह इष्ट कभी
कोई अमरत्व जिसे
सम्मानित करते मानवता सम्मानित हो।
सागर-प्रक्षालित पग,
स्फुर घन उत्तरीय,
वन प्रान्तर जटाजूट,
माथे सूरज उदीय,
...इतना पर्याप्त अभी।
स्मरण में
अमिट स्पर्श निष्कलंक मर्यादाओं के।
बात एक बनने का साहस-सा करती....।
तुम्हारे शब्दों में यदि न कह सकूँ अपनी बात,
विधि-विहीन प्रार्थना
यदि तुम तक न पहुँचे तो
क्षमा कर देना,
मेरे उपकार-मेरे नैवेद्य-
समृद्धियों को छूते हुए
अर्पित होते रहे जिस ईश्वर को
वह यदि अस्पष्ट भी हो
तो ये प्रार्थनाएँ सच्ची हैं...इन्हें
अपनी पवित्रताओं से ठुकराना मत,
चुपचाप विसर्जित हो जाने देना
समय पर....सूर्य पर...
भूख के अनुपयुक्त इस किंचित् प्रसाद को
फिर जूठा मत करना अपनी श्रद्धाओं से,
इनके विधर्म को बचाना अपने शाप से,
इनकी भिक्षुक विनय को छोटा मत करना
अपनी भिक्षा की नाप से
उपेक्षित छोड़ देना
हवाओं पर, सागर पर....
कीर्ति-स्तम्भ वह अस्पष्ट आभा,
सूर्य से सूर्य तक,
प्राण से प्राण तक।
नक्षत्रों,
असंवेद्य विचरण को शीर्षक दो
भीड़-रहित पूजा को फूल दो
तोरण-मण्डप-विहीन मन्दिर को दीपक दो
जबतक मैं न लौटूँ
उपासित रहे वह सब
जिस ओर मेरे शब्दों के संकेत।
जब-जब समर्थ जिज्ञासा से
काल की विदेह अतिशयता को
कोई ललकारे-
सीमा-सन्दर्भहीन साहस को इंगित दो।
पिछली पूजाओं के ये फूटे मंगल-घट।
किसी धर्म-ग्रन्थ के
पृष्ठ-प्रकरण-शीर्षक-
सब अलग-अलग।
वक्ता चढ़ावे के लालच में
बाँच रहे शास्त्र-वचन,
ऊँघ रहे श्रोतागण !...
ओ मस्तक विराट,
इतना अभिमान रहे-
भ्रष्ट अभिषेकों को न दूँ मस्तक
न दूँ मान..
इससे अच्छा
चुपचाप अर्पित हो जा सकूँ
दिगन्त प्रतीक्षाओं को....
अभी नहीं मुकुट और अलंकार।
अभी नहीं तिलक और राज्यभार।
तेजस्वी चिन्तित ललाट। दो मुझको
सदियों तपस्याओं में जी सकने की क्षमता।
पाऊँ कदाचित् वह इष्ट कभी
कोई अमरत्व जिसे
सम्मानित करते मानवता सम्मानित हो।
सागर-प्रक्षालित पग,
स्फुर घन उत्तरीय,
वन प्रान्तर जटाजूट,
माथे सूरज उदीय,
...इतना पर्याप्त अभी।
स्मरण में
अमिट स्पर्श निष्कलंक मर्यादाओं के।
बात एक बनने का साहस-सा करती....।
तुम्हारे शब्दों में यदि न कह सकूँ अपनी बात,
विधि-विहीन प्रार्थना
यदि तुम तक न पहुँचे तो
क्षमा कर देना,
मेरे उपकार-मेरे नैवेद्य-
समृद्धियों को छूते हुए
अर्पित होते रहे जिस ईश्वर को
वह यदि अस्पष्ट भी हो
तो ये प्रार्थनाएँ सच्ची हैं...इन्हें
अपनी पवित्रताओं से ठुकराना मत,
चुपचाप विसर्जित हो जाने देना
समय पर....सूर्य पर...
भूख के अनुपयुक्त इस किंचित् प्रसाद को
फिर जूठा मत करना अपनी श्रद्धाओं से,
इनके विधर्म को बचाना अपने शाप से,
इनकी भिक्षुक विनय को छोटा मत करना
अपनी भिक्षा की नाप से
उपेक्षित छोड़ देना
हवाओं पर, सागर पर....
कीर्ति-स्तम्भ वह अस्पष्ट आभा,
सूर्य से सूर्य तक,
प्राण से प्राण तक।
नक्षत्रों,
असंवेद्य विचरण को शीर्षक दो
भीड़-रहित पूजा को फूल दो
तोरण-मण्डप-विहीन मन्दिर को दीपक दो
जबतक मैं न लौटूँ
उपासित रहे वह सब
जिस ओर मेरे शब्दों के संकेत।
जब-जब समर्थ जिज्ञासा से
काल की विदेह अतिशयता को
कोई ललकारे-
सीमा-सन्दर्भहीन साहस को इंगित दो।
पिछली पूजाओं के ये फूटे मंगल-घट।
किसी धर्म-ग्रन्थ के
पृष्ठ-प्रकरण-शीर्षक-
सब अलग-अलग।
वक्ता चढ़ावे के लालच में
बाँच रहे शास्त्र-वचन,
ऊँघ रहे श्रोतागण !...
ओ मस्तक विराट,
इतना अभिमान रहे-
भ्रष्ट अभिषेकों को न दूँ मस्तक
न दूँ मान..
इससे अच्छा
चुपचाप अर्पित हो जा सकूँ
दिगन्त प्रतीक्षाओं को....
वाजश्रवा
अत्र उसन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ।
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस।
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस।
पिता, तुम भविष्य के अधिकारी नहीं,
क्योंकि तुम ‘अपने’ हित के आगे नहीं सोच पा रहे,
न अपने ‘हित’ को ही अपने सुख के आगे।
तुम वर्तमान को संज्ञा देते हो, पर महत्त्व नहीं।
तुम्हारे पास जो है, उसे ही बार-बार पाते हो
और सिद्ध नहीं कर पाते कि उसने
तुम्हें सन्तुष्ट किया।
इसीलिए तुम्हारी देन से तुम्हारी ही तरह फिर पानेवाला तृप्त नहीं होता,
तुम्हारे पास जो है, उससे और अधिक चाहता है,
विश्वास नहीं करता कि तुम इतना ही दे सकते हो।
पिता, तुम भविष्य के अधिकारी नहीं, क्योंकि
तुम्हारा वर्तमान जिस दिशा में मुड़ता है
वहां कहीं एक भयानक शत्रु है जो तुम्हें मारकर तुम्हारे संचयों को तुम्हारे ही मार्ग में ही लूट लेता है, और तुम खाली हाथ लौट आते हो।
क्योंकि तुम ‘अपने’ हित के आगे नहीं सोच पा रहे,
न अपने ‘हित’ को ही अपने सुख के आगे।
तुम वर्तमान को संज्ञा देते हो, पर महत्त्व नहीं।
तुम्हारे पास जो है, उसे ही बार-बार पाते हो
और सिद्ध नहीं कर पाते कि उसने
तुम्हें सन्तुष्ट किया।
इसीलिए तुम्हारी देन से तुम्हारी ही तरह फिर पानेवाला तृप्त नहीं होता,
तुम्हारे पास जो है, उससे और अधिक चाहता है,
विश्वास नहीं करता कि तुम इतना ही दे सकते हो।
पिता, तुम भविष्य के अधिकारी नहीं, क्योंकि
तुम्हारा वर्तमान जिस दिशा में मुड़ता है
वहां कहीं एक भयानक शत्रु है जो तुम्हें मारकर तुम्हारे संचयों को तुम्हारे ही मार्ग में ही लूट लेता है, और तुम खाली हाथ लौट आते हो।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i