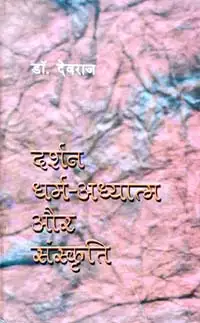|
कविता संग्रह >> इतिहास-पुरुष इतिहास-पुरुषदेवराज
|
291 पाठक हैं |
|||||||
‘इतिहास-पुरुष’ प्रख्यात दर्शन-वेत्ता, कवि, समालोचक और चिन्तक डॉ. देवराज का लघु-काव्य अपनी लघुता में भी विराट है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘इतिहास-पुरुष’ प्रख्यात दर्शन-वेत्ता, कवि, समालोचक
और चिन्तक डॉ. देवराज का लघु-काव्य अपनी लघुता में भी विराट है। मनुष्य
जीवन के पूर्वापर, उसके आगत-अनागत, वांछित-अवांछित, ज्ञेय-अज्ञेय को काव्य
में ढालने का ऋषि प्रयास है-‘इतिहास-पुरुष’।
आज का मानव ज्ञान-विज्ञान और प्रावधिकी में उन्नत होने के बावजूद सुखी-सन्तुष्ट और प्रसन्न नजर नहीं आता। वह जीने की कला भूल चुका है। मनुष्य का मन अद्भुत अन्तर्विरोधी से ग्रस्त है। ‘इतिहास-पुरुष’ इस द्वन्द्वबोध से ग्रस्त मनुष्य को मानवीय धरातल पर पूरे उत्साह से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। देखा जाए तो इस कृति में गीता के निष्काम कर्म का सन्देश निहित है। कवि ने अमूर्त्त को रूपायित करके ब्रह्म को इतिहास-पुरुष के रूप में लोकमंगल और प्रगतिशील चेतना की भावमूर्ति प्रदान करके विश्व-सौन्दर्य से मण्डित कर दिया है। इस लघु-काव्य में डॉ. देवराज ने अपनी सृजनात्मक मानववाद की परिकल्पना तथा भौतिकता और अध्यात्म के सम्यक् समन्वय का अनूठा दर्शन प्रस्तुत किया है।
ऐसी महत्वपूर्ण कृति को नव परिवर्धन के साथ प्रकाशित कर पाठकों को सौंपते हुए भारतीय ज्ञानपीठ को प्रसन्नता है।
आज का मानव ज्ञान-विज्ञान और प्रावधिकी में उन्नत होने के बावजूद सुखी-सन्तुष्ट और प्रसन्न नजर नहीं आता। वह जीने की कला भूल चुका है। मनुष्य का मन अद्भुत अन्तर्विरोधी से ग्रस्त है। ‘इतिहास-पुरुष’ इस द्वन्द्वबोध से ग्रस्त मनुष्य को मानवीय धरातल पर पूरे उत्साह से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। देखा जाए तो इस कृति में गीता के निष्काम कर्म का सन्देश निहित है। कवि ने अमूर्त्त को रूपायित करके ब्रह्म को इतिहास-पुरुष के रूप में लोकमंगल और प्रगतिशील चेतना की भावमूर्ति प्रदान करके विश्व-सौन्दर्य से मण्डित कर दिया है। इस लघु-काव्य में डॉ. देवराज ने अपनी सृजनात्मक मानववाद की परिकल्पना तथा भौतिकता और अध्यात्म के सम्यक् समन्वय का अनूठा दर्शन प्रस्तुत किया है।
ऐसी महत्वपूर्ण कृति को नव परिवर्धन के साथ प्रकाशित कर पाठकों को सौंपते हुए भारतीय ज्ञानपीठ को प्रसन्नता है।
निवेदन
कुछ वर्ष पूर्व अँग्रेजी
‘पार्नासस’ पुस्तक, जिसमें
तरह-तरह की-कथात्मक, चिन्तनात्मक, व्यंग्यमू्लक, शिक्षापरक आदि-मुख्यत:
लम्बी कविताओं का संकलन है, देखकर यह भावना हुई थी कि उस कोटि के कुछ
प्रयास किए जाएँ। ‘पार्नासस’ में संगृहीत कृतियों में
समय, भाषा, शैली आदि की बड़ी विविधता है; समानता एक ही है-वे सब अपने-अपने
ढंग से सुसंगठित एवं कथ्य तथा शैली की दृष्टि से प्रौढ़ रचनाएँ हैं। उक्त
भावना या विचार ने, कुछ दूसरी प्रेरणाओं के साथ मिलकर, मुझे
‘इतिहास-पुरुष’ लिखने की ओर उन्मुख किया। यह छोटा-सा
काव्य सन् ’61 और ’62 की गरमी की छुट्टियों में लिखा
गया; ‘नूरजहाँ’ जून 64 में, और
‘क्लिओपेट्रा का पत्र’ सम्भवत: जनवरी ’63
में।
प्रस्तुत लेखक को अपना समय, विश्वविद्यालय की नौकरी के अलावा, साहित्य और दर्शन के बीच विभक्त करना पड़ता है; उसके शैलीकार का अवधान और शक्ति भी हिन्दी-अँग्रेजी के बीच बँट जाती है। इस जीवन में इन द्वन्द्वों की स्थिति से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं दीखता।
लेकिन मेरे साहित्य में मेरा दर्शन दोहराया जाता हो, ऐसा अनुभव मुझे नहीं है। ‘संस्कृति का दार्शनिक विवेचन’ पहले लिखा गया था, और लम्बे-चौड़े चिन्तन के बाद, किन्तु ‘इतिहास-पुरुष’ की केन्द्रगत दृष्टि वहाँ से उठाई गयी या उसका अनुवाद-मात्र नहीं है। सम्भवत: आगे की किसी रचना में वह दृष्टि अब इतने आटोप और सतर्कता से जगह नहीं पाएगी। सच यह है कि साहित्यगत चिन्तन को उसके प्राणभूत ऐन्द्रिय-बोध एवं भाव-सामग्री से जुदा नहीं किया जा सकता। यों किसी भी ईमानदार एवं व्यक्तित्व-सम्पन्न लेखक की विविध रचनाओं में मौलिक एकता-विकासमान एकसूत्रता-प्रतिपलित होनी ही चाहिए।
इस काव्य को लिखते-दोहराते हुए मैंने अनेक अवसरों पर, आश्चर्य और खेद के साथ, तीखे रूप में अनुभव किया है कि एक छोटी-सी कृति को भी निर्दोष, सर्वांश में ग्राह्य रूप देना कितना कठिन कार्य है; ऐसे अवसरों पर मुझे ‘मेघदूत’ जैसी कृतियों के रचयिताओं से सहज ही ईर्ष्या महसूस हुई है। शायद उसी अनुपात में उनके प्रति आदर का भाव, और अधिक सचेत व परिश्रमशील होने का संकल्प भी दृढ़ हुआ है।
हिन्दी के साहित्य-प्रेमियों के बीच प्रस्तुत लेखक अपनी क्लासिसिज़्म-क्लासिकी (श्रेण्य) लेखकों के पक्षपात- के लिए ख्यात या बदनाम है, पर इसमें सन्देह है कि उसकी क्लासिकीयता की धारणा भी उतनी ही सुविदित है। मेरी उक्त धारणा का क्लासिक-रोमैण्टिक के ऐतिहासिक झगड़े से विशेष लगाव नहीं है। मेरी दृष्टि से क्लासिक कोटि की कृति वह है जिसमें (1) एक प्रकार की पूर्णता, भावों का पूरा परिपाक (एफ्.आर.लीविस के शब्दों में ‘रिअलाइज़ेशन’) और अभिव्यक्तिगत प्रौढ़ता तथा (2) रागतत्त्व और बोधतत्त्व (विभावों, इलियट के सह-अपेक्षी वस्तु-विन्यास) की समशक्तिता या आन्तरिक सामंजस्य हो। मैं यह भी मानता हूँ कि अच्छा और प्राणवान् साहित्य रोचक या अर्थपूर्ण सन्दर्भों के निर्माण में ही अस्तित्व लाभ करता है। ऐसे सन्दर्भों का निर्माण रचनाकार में सशक्त नियन्त्रक बुद्धि के अलावा उन वृत्तियों की अपेक्षा करता है जिन्हें इधर के समीक्षक-विचारकों ने संसक्ति (इन्वॉल्वमेण्ट) और प्रतिबद्धता (कॅमिटमेण्ट) की आख्याएँ दी हैं। (संसक्ति से मैं समझता हूँ जीवन और उसके मूल्यों में गहरी, जीवन्त, अभिरुचि; प्रतिबद्धता से मतलब है देखे हुए मूल्यों के प्रभावपूर्ण उल्लेख और उन्हें सामाजिकों अथवा सहधर्मियों के द्वारा ग्राह्य बनाने के लिए बेचैनी। प्रतिबद्ध होने का अर्थ आवश्यक रूप में बहिर्मुख, अथवा स्थूल रूप में कर्मठ, होना नहीं है।) इन वृत्तियों की अपेक्षा दो कारणों से है : एक, संसक्त और प्रतिबद्ध कलाकार ही जीवन-अनुभूति के विभिन्न आयामों से, सामान्य (नॉर्मल) संवेदना के धरातल पर, साक्षात् परिचय कर पाता है; इस परिचय में ही उसे भावबोध के तत्त्व निहित रहते हैं जो साहित्यगत चेतना का ग्रथन करते हैं। उदाहरण : जिस व्यक्ति ने कभी मन-प्राण से प्रेम किया है, वही सफल और समृद्ध प्रेमकाव्य लिख सकता है; और जिसने निर्णय और कर्म के विविध अवसरों पर नैतिक द्वन्द्वों को अपने रक्त में जाना-सहा है, वही उन्हें तीखी साहित्यिक अभिव्यक्ति दे सकता है। एक सच्चे व गहरे अर्थ में देशप्रेमी कवि ही देश को लेकर अर्थ-सम्पन्न रचनाएँ प्रस्तुत कर सकता है। निष्कर्ष यह कि समृद्ध जीवन-संसक्ति (फिर भले ही वह मात्र सशक्त कल्पना के धरातल पर हो) सम्पन्न साहित्य-सृजन की आवश्यक शर्त है। मूल्यों के विघटन की चेतना वहीं तक लेखक की रचना को समृद्ध करती है, जहाँ तक उसका उदय जीवन के विस्तृत व सार्थक उपभोग की माँग में होता है। दूसरे, जहाँ लेखक की संसक्ति उसके कृतित्व को आन्तरिक ऐक्य देती हैं, वहाँ प्रतिबद्धता का आवेग उसे अधिक सृजनशील बनाता है, और उसकी रचना को अधिक शक्तिपूर्ण। कहने की जरूरत नहीं कि रचना की दृष्टि से उपयोगी संसक्ति और प्रतिबद्धता लेखक द्वारा उपार्जित दृष्टि व साक्षात्कार का परिणाम होती है- किसी बाहरी स्रोत से पकड़ी हुई अमूर्त सिद्धान्तवादिता या कट्टरता नहीं। यही कारण है कि साधनाशील लेखक की दृष्टि का प्रकाशन सहज ही उपयुक्त चित्र-सामग्री और भावबोध से अलंकृत हो उठता है।
किसी भी उल्लेख्य लेखक पर उस समूचे अतीत का आभार रहता है जिससे आलाप-संलाप करते हुए उसकी चेतना गठित होती है। सचेत रूप में, प्रस्तुत लेखक ‘ग्राम्या’ के पन्त और अज्ञेय की भाषा का विशेष प्रशंसक रहा है; निश्चय ही वह अपने शब्दों-सम्बन्धों बोध और प्रयोग में उनसे प्रभावित हुआ होगा। उसने ‘कला और बूढ़ा चाँद’ के शब्द-विन्यास की नयी क़िस्म की ताजगी से भी चमत्कृत महसूस किया था। इसके अलावा वह क्लासिकी संस्कृत साहित्य, उर्दू ग़ज़ल, कतिपय फ्रांसीसी (क्लासिकी) नाटककारों और अँग्रेजी के कवियों से विशेष प्रेरणा लेता रहा है।
इतिहास-पुरुष के छन्द की प्रेरणा सम्भवत: प्रथम ‘तार सप्तक’ में संग्रहीत श्री प्रभाकर माचवे की एक कविता (‘नोन-तेल-लकड़ी की फ़िक्र में लगे घुन से’) से मिली थी, यों उक्त रचना में प्रयुक्त छन्द के अनेक प्रतिरूप (वेरिएण्ट्स) मिल सकेंगे, जैसे-
प्रस्तुत लेखक को अपना समय, विश्वविद्यालय की नौकरी के अलावा, साहित्य और दर्शन के बीच विभक्त करना पड़ता है; उसके शैलीकार का अवधान और शक्ति भी हिन्दी-अँग्रेजी के बीच बँट जाती है। इस जीवन में इन द्वन्द्वों की स्थिति से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं दीखता।
लेकिन मेरे साहित्य में मेरा दर्शन दोहराया जाता हो, ऐसा अनुभव मुझे नहीं है। ‘संस्कृति का दार्शनिक विवेचन’ पहले लिखा गया था, और लम्बे-चौड़े चिन्तन के बाद, किन्तु ‘इतिहास-पुरुष’ की केन्द्रगत दृष्टि वहाँ से उठाई गयी या उसका अनुवाद-मात्र नहीं है। सम्भवत: आगे की किसी रचना में वह दृष्टि अब इतने आटोप और सतर्कता से जगह नहीं पाएगी। सच यह है कि साहित्यगत चिन्तन को उसके प्राणभूत ऐन्द्रिय-बोध एवं भाव-सामग्री से जुदा नहीं किया जा सकता। यों किसी भी ईमानदार एवं व्यक्तित्व-सम्पन्न लेखक की विविध रचनाओं में मौलिक एकता-विकासमान एकसूत्रता-प्रतिपलित होनी ही चाहिए।
इस काव्य को लिखते-दोहराते हुए मैंने अनेक अवसरों पर, आश्चर्य और खेद के साथ, तीखे रूप में अनुभव किया है कि एक छोटी-सी कृति को भी निर्दोष, सर्वांश में ग्राह्य रूप देना कितना कठिन कार्य है; ऐसे अवसरों पर मुझे ‘मेघदूत’ जैसी कृतियों के रचयिताओं से सहज ही ईर्ष्या महसूस हुई है। शायद उसी अनुपात में उनके प्रति आदर का भाव, और अधिक सचेत व परिश्रमशील होने का संकल्प भी दृढ़ हुआ है।
हिन्दी के साहित्य-प्रेमियों के बीच प्रस्तुत लेखक अपनी क्लासिसिज़्म-क्लासिकी (श्रेण्य) लेखकों के पक्षपात- के लिए ख्यात या बदनाम है, पर इसमें सन्देह है कि उसकी क्लासिकीयता की धारणा भी उतनी ही सुविदित है। मेरी उक्त धारणा का क्लासिक-रोमैण्टिक के ऐतिहासिक झगड़े से विशेष लगाव नहीं है। मेरी दृष्टि से क्लासिक कोटि की कृति वह है जिसमें (1) एक प्रकार की पूर्णता, भावों का पूरा परिपाक (एफ्.आर.लीविस के शब्दों में ‘रिअलाइज़ेशन’) और अभिव्यक्तिगत प्रौढ़ता तथा (2) रागतत्त्व और बोधतत्त्व (विभावों, इलियट के सह-अपेक्षी वस्तु-विन्यास) की समशक्तिता या आन्तरिक सामंजस्य हो। मैं यह भी मानता हूँ कि अच्छा और प्राणवान् साहित्य रोचक या अर्थपूर्ण सन्दर्भों के निर्माण में ही अस्तित्व लाभ करता है। ऐसे सन्दर्भों का निर्माण रचनाकार में सशक्त नियन्त्रक बुद्धि के अलावा उन वृत्तियों की अपेक्षा करता है जिन्हें इधर के समीक्षक-विचारकों ने संसक्ति (इन्वॉल्वमेण्ट) और प्रतिबद्धता (कॅमिटमेण्ट) की आख्याएँ दी हैं। (संसक्ति से मैं समझता हूँ जीवन और उसके मूल्यों में गहरी, जीवन्त, अभिरुचि; प्रतिबद्धता से मतलब है देखे हुए मूल्यों के प्रभावपूर्ण उल्लेख और उन्हें सामाजिकों अथवा सहधर्मियों के द्वारा ग्राह्य बनाने के लिए बेचैनी। प्रतिबद्ध होने का अर्थ आवश्यक रूप में बहिर्मुख, अथवा स्थूल रूप में कर्मठ, होना नहीं है।) इन वृत्तियों की अपेक्षा दो कारणों से है : एक, संसक्त और प्रतिबद्ध कलाकार ही जीवन-अनुभूति के विभिन्न आयामों से, सामान्य (नॉर्मल) संवेदना के धरातल पर, साक्षात् परिचय कर पाता है; इस परिचय में ही उसे भावबोध के तत्त्व निहित रहते हैं जो साहित्यगत चेतना का ग्रथन करते हैं। उदाहरण : जिस व्यक्ति ने कभी मन-प्राण से प्रेम किया है, वही सफल और समृद्ध प्रेमकाव्य लिख सकता है; और जिसने निर्णय और कर्म के विविध अवसरों पर नैतिक द्वन्द्वों को अपने रक्त में जाना-सहा है, वही उन्हें तीखी साहित्यिक अभिव्यक्ति दे सकता है। एक सच्चे व गहरे अर्थ में देशप्रेमी कवि ही देश को लेकर अर्थ-सम्पन्न रचनाएँ प्रस्तुत कर सकता है। निष्कर्ष यह कि समृद्ध जीवन-संसक्ति (फिर भले ही वह मात्र सशक्त कल्पना के धरातल पर हो) सम्पन्न साहित्य-सृजन की आवश्यक शर्त है। मूल्यों के विघटन की चेतना वहीं तक लेखक की रचना को समृद्ध करती है, जहाँ तक उसका उदय जीवन के विस्तृत व सार्थक उपभोग की माँग में होता है। दूसरे, जहाँ लेखक की संसक्ति उसके कृतित्व को आन्तरिक ऐक्य देती हैं, वहाँ प्रतिबद्धता का आवेग उसे अधिक सृजनशील बनाता है, और उसकी रचना को अधिक शक्तिपूर्ण। कहने की जरूरत नहीं कि रचना की दृष्टि से उपयोगी संसक्ति और प्रतिबद्धता लेखक द्वारा उपार्जित दृष्टि व साक्षात्कार का परिणाम होती है- किसी बाहरी स्रोत से पकड़ी हुई अमूर्त सिद्धान्तवादिता या कट्टरता नहीं। यही कारण है कि साधनाशील लेखक की दृष्टि का प्रकाशन सहज ही उपयुक्त चित्र-सामग्री और भावबोध से अलंकृत हो उठता है।
किसी भी उल्लेख्य लेखक पर उस समूचे अतीत का आभार रहता है जिससे आलाप-संलाप करते हुए उसकी चेतना गठित होती है। सचेत रूप में, प्रस्तुत लेखक ‘ग्राम्या’ के पन्त और अज्ञेय की भाषा का विशेष प्रशंसक रहा है; निश्चय ही वह अपने शब्दों-सम्बन्धों बोध और प्रयोग में उनसे प्रभावित हुआ होगा। उसने ‘कला और बूढ़ा चाँद’ के शब्द-विन्यास की नयी क़िस्म की ताजगी से भी चमत्कृत महसूस किया था। इसके अलावा वह क्लासिकी संस्कृत साहित्य, उर्दू ग़ज़ल, कतिपय फ्रांसीसी (क्लासिकी) नाटककारों और अँग्रेजी के कवियों से विशेष प्रेरणा लेता रहा है।
इतिहास-पुरुष के छन्द की प्रेरणा सम्भवत: प्रथम ‘तार सप्तक’ में संग्रहीत श्री प्रभाकर माचवे की एक कविता (‘नोन-तेल-लकड़ी की फ़िक्र में लगे घुन से’) से मिली थी, यों उक्त रचना में प्रयुक्त छन्द के अनेक प्रतिरूप (वेरिएण्ट्स) मिल सकेंगे, जैसे-
बाँधते न क्यों मन को दवा क्यों न कर
पाते
ऊब औ’ उचाटों की
का ध्वनि-संयोजन जिग़र की ‘अब कहाँ
ज़माने में दूसरा जवाब
उनका’ और ग़ालिब की ‘हम कहाँ के दाना थे किस हुनर में
यकता थे’1 पंक्तियों के ज़्यादा करीब है और ‘सत-रज-तम
तीनों के रूप-गन्ध-रंग लिये’ से काफ़ी भिन्न; यही बात अनेकविध
दूसरी-चौथी पंक्तियों पर भी लागू होगी।
------------------------------
1.मुझे उर्दू ग़ज़ल की भाषा और लहजा एक श्लाघनीय अर्थ में आधुनिक लगता है। अधिकांश नयी कविता की उखड़ी-पुखड़ी नवीनता की तुलना में उसका अनुशासित, स्थिर आधुनिकता का स्वर मुझे अधिक भाता है।
ओवेन बारफ़ील्ड ने अपनी पुस्तक ‘पोएटिक डिक्शन’ में काव्यगत चेतना की अपरिचितता (स्ट्रेंजनेस) के महत्त्व को विशेष गौरव दिया है। हमारा अनुमान है कि यह विशेषता पूरी-पूरी प्राचीनों के ‘चमत्कार’ में अन्तर्भुक्त हो जाती है; इधर की नयेपन की माँग भी एक हद तक उसी चीज की माँग है-चमत्कार की। मेरा विचार है कि, विभिन्न स्थितियों में, उक्त विशेषता के अलग-अलग उपादान होते हैं-अनुप्रास, सटीक औचित्य, अर्थगौरव, अभिव्यक्ति का अप्रत्याशित संक्षेप और उसकी सघनता, चित्रसामग्री की आकर्षकता, आदि। इधर कहा गया है कि श्रेष्ठ रचनाकार शब्दों के परम्पराभुक्त अर्थ में परिवर्तन उपस्थित करके अभ्यस्त प्रतिक्रिया (स्टॉक रेसपान्स) को निरूद्ध करता है; मेरे खयाल में यह निरोध समर्थ नये सन्दर्भ द्वारा स्वत: उत्पन्न हो जाता है। मैं यह भी स्वीकार नहीं करता कि नयेपन, चमत्कार या अपरिचितता की संवेदना जगाने का कोई एक रूढ़ तरीक़ा होता है- जैसा कि कतिपय साहित्यिक निकाय प्रचारित करते हैं। ये निकाय साहित्य की ऐतिहासिक विविधता और पुरानी कृतियों की सदाबहार आकर्षकता की कोई संगत व्याख्या नहीं दे सकते। साथ ही यह देखा जाता है कि रूढ़ तरीक़ों का सहारा लेनेवाले सम्प्रदायवादी लेखक प्राय: व्यक्तित्व-सम्पन्न नहीं हो पाते, वे प्रचलित काव्य-भाषा के मुहावरे में एकरसता के प्रसार का अन्यतम कारण भी बन जाते हैं।
साहित्य के इतिहास का सबसे बड़ा आश्चर्य है- उसकी महनीय कृतियों का कभी न चुकनेवाला आकर्षण। और यह आकर्षण तरह-तरह का होता है: चित्रसामग्री का (नासा मोरि नचाय दृग); अनुप्रास का (करी कका की सौंह, काँटे-सी कसकति हिये वहै कटीली भौंह); सन्दर्भ-नियन्त्रित सटीक उक्ति का (पुनि आउब इहिं बिरियाँ काली, अस कह मन बिहँसी इक आली); अभिव्यक्ति की जटिल या सघन पूर्णता का (‘बृहद जिह्म विश्लथ केंचुल-सा लगता चितकबरा गंगाजल’; अथवा ‘जनमन में तुम कर सको वहन मेरे विचार’; अथवा ‘आ गये प्रियंवद, केशकम्बली, गुफागेह’); और कभी-कभी एकदम सीधी स्वभावोक्ति (?) का (सूरदास को ठाकुर ठाड़ो हाथ लकुट लिये छोटी), इत्यादि । ऐसी स्थिति में काव्यगत सौन्दर्य के किसी एक उपादान पर ऐकान्तिक ज़ोर देना-एकत्ववाद-मुझे पसन्द नहीं आता। यह भी ठीक है कि महत्त्वपूर्ण नवीन लेखक इन उपादानों या तरीक़ों में अनजाने नये तत्त्व जोड़ते रहते हैं; अच्छे लेखक प्राय: एक साथ अनेक वैसे तत्त्वों, उपादानों या तरीक़ों का उपयोग करते हैं।
इस संग्रह की प्राय: सभी रचनाएँ सन् ’60 के बाद की हैं, इसका एकमात्र अपवाद ‘ऋष्य श्रृंग’ है, जो सन् ’40 के आसपास लिखी गयी थी। ‘उर्वशी ने कहा’ में संकलित ‘शिव का मत्स्याखेट’ भी तभी की रचना है। ‘ऋष्य श्रृंग’ वय: सन्धि के पाठकों के लिए है, वैसे ही जैसे ‘मत्स्याखेट’ बाल-सुलभ कुतूहलवाले पाठकों के लिए थी। यों मेरा विश्वास है कि अभ्यस्त साहित्यिक पाठक कभी इतना ‘वृद्ध’ नहीं होता कि उक्त धरातलों पर संक्रमण न कर सके। मेरे विकास का आभास देने के अतिरिक्त ये रचनाएँ एक दूसरी दृष्टि से उपयोगी हो सकती हैं-साहित्य-चिन्तकों द्वारा प्रौढ़ता की दिशाओं की खोज करने में।1
अन्त में, मैं आदरणीय कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त के प्रति, उनके द्वारा लिखे ‘इतिहास-पुरुष’ के प्राक्कथन के लिए, विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ‘पल्लव’, ‘गुंजन’, ‘ग्राम्या’ तथा ‘कला और बूढ़ा चाँद’ जैसी कृतियों में हिन्दी काव्यभाषा को अनेक नये आयामों से परिचित करानेवाले उक्त कवि को- जो, स्रष्टा-द्रष्टा के रूप में, दो महत्त्वपूर्ण रचना-युगों से सम्बद्ध रहा है-इस संग्रह की यह प्रमुख रचना प्रिय लगी यह मेरे लिए विशेष परितोष की बात है। यों मैं पाठकों को सूचित करूँ कि संकेताधीन रचना एक नयी दिशा में लेखक का पहला प्रयास है। उसे विश्वास है कि पन्त जी तथा दूसरों का समुचित प्रोत्साहन उसके आगे आनेवाले प्रयत्नों को अधिक आत्मविश्वास और सतर्क साहस का सम्बल देगा।
------------------------------
1.मुझे उर्दू ग़ज़ल की भाषा और लहजा एक श्लाघनीय अर्थ में आधुनिक लगता है। अधिकांश नयी कविता की उखड़ी-पुखड़ी नवीनता की तुलना में उसका अनुशासित, स्थिर आधुनिकता का स्वर मुझे अधिक भाता है।
ओवेन बारफ़ील्ड ने अपनी पुस्तक ‘पोएटिक डिक्शन’ में काव्यगत चेतना की अपरिचितता (स्ट्रेंजनेस) के महत्त्व को विशेष गौरव दिया है। हमारा अनुमान है कि यह विशेषता पूरी-पूरी प्राचीनों के ‘चमत्कार’ में अन्तर्भुक्त हो जाती है; इधर की नयेपन की माँग भी एक हद तक उसी चीज की माँग है-चमत्कार की। मेरा विचार है कि, विभिन्न स्थितियों में, उक्त विशेषता के अलग-अलग उपादान होते हैं-अनुप्रास, सटीक औचित्य, अर्थगौरव, अभिव्यक्ति का अप्रत्याशित संक्षेप और उसकी सघनता, चित्रसामग्री की आकर्षकता, आदि। इधर कहा गया है कि श्रेष्ठ रचनाकार शब्दों के परम्पराभुक्त अर्थ में परिवर्तन उपस्थित करके अभ्यस्त प्रतिक्रिया (स्टॉक रेसपान्स) को निरूद्ध करता है; मेरे खयाल में यह निरोध समर्थ नये सन्दर्भ द्वारा स्वत: उत्पन्न हो जाता है। मैं यह भी स्वीकार नहीं करता कि नयेपन, चमत्कार या अपरिचितता की संवेदना जगाने का कोई एक रूढ़ तरीक़ा होता है- जैसा कि कतिपय साहित्यिक निकाय प्रचारित करते हैं। ये निकाय साहित्य की ऐतिहासिक विविधता और पुरानी कृतियों की सदाबहार आकर्षकता की कोई संगत व्याख्या नहीं दे सकते। साथ ही यह देखा जाता है कि रूढ़ तरीक़ों का सहारा लेनेवाले सम्प्रदायवादी लेखक प्राय: व्यक्तित्व-सम्पन्न नहीं हो पाते, वे प्रचलित काव्य-भाषा के मुहावरे में एकरसता के प्रसार का अन्यतम कारण भी बन जाते हैं।
साहित्य के इतिहास का सबसे बड़ा आश्चर्य है- उसकी महनीय कृतियों का कभी न चुकनेवाला आकर्षण। और यह आकर्षण तरह-तरह का होता है: चित्रसामग्री का (नासा मोरि नचाय दृग); अनुप्रास का (करी कका की सौंह, काँटे-सी कसकति हिये वहै कटीली भौंह); सन्दर्भ-नियन्त्रित सटीक उक्ति का (पुनि आउब इहिं बिरियाँ काली, अस कह मन बिहँसी इक आली); अभिव्यक्ति की जटिल या सघन पूर्णता का (‘बृहद जिह्म विश्लथ केंचुल-सा लगता चितकबरा गंगाजल’; अथवा ‘जनमन में तुम कर सको वहन मेरे विचार’; अथवा ‘आ गये प्रियंवद, केशकम्बली, गुफागेह’); और कभी-कभी एकदम सीधी स्वभावोक्ति (?) का (सूरदास को ठाकुर ठाड़ो हाथ लकुट लिये छोटी), इत्यादि । ऐसी स्थिति में काव्यगत सौन्दर्य के किसी एक उपादान पर ऐकान्तिक ज़ोर देना-एकत्ववाद-मुझे पसन्द नहीं आता। यह भी ठीक है कि महत्त्वपूर्ण नवीन लेखक इन उपादानों या तरीक़ों में अनजाने नये तत्त्व जोड़ते रहते हैं; अच्छे लेखक प्राय: एक साथ अनेक वैसे तत्त्वों, उपादानों या तरीक़ों का उपयोग करते हैं।
इस संग्रह की प्राय: सभी रचनाएँ सन् ’60 के बाद की हैं, इसका एकमात्र अपवाद ‘ऋष्य श्रृंग’ है, जो सन् ’40 के आसपास लिखी गयी थी। ‘उर्वशी ने कहा’ में संकलित ‘शिव का मत्स्याखेट’ भी तभी की रचना है। ‘ऋष्य श्रृंग’ वय: सन्धि के पाठकों के लिए है, वैसे ही जैसे ‘मत्स्याखेट’ बाल-सुलभ कुतूहलवाले पाठकों के लिए थी। यों मेरा विश्वास है कि अभ्यस्त साहित्यिक पाठक कभी इतना ‘वृद्ध’ नहीं होता कि उक्त धरातलों पर संक्रमण न कर सके। मेरे विकास का आभास देने के अतिरिक्त ये रचनाएँ एक दूसरी दृष्टि से उपयोगी हो सकती हैं-साहित्य-चिन्तकों द्वारा प्रौढ़ता की दिशाओं की खोज करने में।1
अन्त में, मैं आदरणीय कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त के प्रति, उनके द्वारा लिखे ‘इतिहास-पुरुष’ के प्राक्कथन के लिए, विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ‘पल्लव’, ‘गुंजन’, ‘ग्राम्या’ तथा ‘कला और बूढ़ा चाँद’ जैसी कृतियों में हिन्दी काव्यभाषा को अनेक नये आयामों से परिचित करानेवाले उक्त कवि को- जो, स्रष्टा-द्रष्टा के रूप में, दो महत्त्वपूर्ण रचना-युगों से सम्बद्ध रहा है-इस संग्रह की यह प्रमुख रचना प्रिय लगी यह मेरे लिए विशेष परितोष की बात है। यों मैं पाठकों को सूचित करूँ कि संकेताधीन रचना एक नयी दिशा में लेखक का पहला प्रयास है। उसे विश्वास है कि पन्त जी तथा दूसरों का समुचित प्रोत्साहन उसके आगे आनेवाले प्रयत्नों को अधिक आत्मविश्वास और सतर्क साहस का सम्बल देगा।
देवराज
-----------------------------
1.मूल निवेदन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित ‘इतिहास-पुरुष तथा अन्य कविताएँ’ संकलन की प्रस्तावना के रूप में लिखा गया था।
1.मूल निवेदन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित ‘इतिहास-पुरुष तथा अन्य कविताएँ’ संकलन की प्रस्तावना के रूप में लिखा गया था।
प्राक्कथन
‘इतिहास-पुरुष’ नयी
कविता का एक उत्कृष्टतम काव्य है।
लय-छन्द में रचित, प्रगीतों की स्वर्णश्रृंखला में गुम्फित यह लघु काव्य
अपने सन्तुलित शिल्प तथा उर्वर आढ्य कथ्य के कारण नयी कविता के उन सभी
दोषों से मुक्त है, जो उसमें बिखराव पैदा कर उसे मात्र एक खोखला अलंकरण
बना देते हैं। ऐसी उच्च कोटि की कृति के सृजन के लिए सूक्ष्म कला-बोध तथा
व्यापक जीवन अनुभूति के अतिरिक्त इतिहास-दर्शन तथा विश्व के अन्तर्विधान
में गम्भीर मर्मभेदिनी दृष्टि की भी आवश्यकता होती है जो डॉ. देवराज के
पास प्रचुर मात्रा में वर्तमान है।
‘इतिहास-पुरुष’ तीन भागों में विभक्त है। पहला भाग है, ‘परिचय’ जिसमें इतिहास-पुरुष नाटकीय गरिमा के साथ अपने स्वरूप का परिचय देता है। इस खण्ड में कवि ने निर्जीव यान्त्रिक कला-संचरण को विश्वात्मा का अमरत्व तथा जीवन चैतन्य का ऐश्वर्य प्रदान कर, उसके विभिन्न आयामों को अत्यन्त सशक्त एवं कलात्मक ढंग से चित्रित कर, लोकोत्तर चमत्कार पैदा कर दिया है। अपनी भूत-वर्तमान की उपलब्धियों तथा भावी सम्भावनाओं का उद्घाटन इतिहास-पुरुष जिस कवित्वपूर्ण राजसी ढंग से करता है, उसके गौरव से अभिभूत मन को सचमुच ही निष्कल निष्प्रपंच, क्रिया-गुणों से वर्जित अशरीरी ब्रह्म की कल्पना नीरस तथा निस्सार प्रतीत होने लगती है। निश्चय ही कवि ने अपनी अन्त:स्पर्शी प्रतिभा और विराट् ऋत कल्पना से अमूर्त ब्रह्म को इतिहास-पुरुष के रूप में लोकमंगलमय, जीवनमांसल रूप देकर, उसे सगुण, प्रगतिशील तथा भावमूर्त कर वैश्व सौन्दर्य से मण्डित कर दिया है। ऐसा लगता है कि शतियों की सौ करोड़ शाखाओं में बृहद् व्यापक इस विशाल वट पादप की स्वप्न मौन छाँह में खड़ा प्रबुद्धचेता रसवर्षी कवि विकासशील सृष्टि-तत्त्व का हस्तामलकवत् आर-पार निरीक्षण कर उसे जरारोगहीन अमर अनादि काल-विष्णु की गहरी नाभि-गुहा से निकले सहस्रनेत्र ब्रह्मकमल-स्वरूप इतिहास-पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है, जिसमें केवल दिक्सर्जित व्याप्ति ही नहीं, उद्बुद्ध लोक-जीवन की भावना-मनीषा में बहनेवाला अन्तर्लीन जाज्ज्वल्यमान तेज भी है। नि:सन्देह, इतिहास-पुरुष की चेतना से संयुक्त होकर ही मनुष्य जीवन तथा सृष्टि का अखण्ड प्रयोजन समझ सकता है, जैसा कि वह सृष्टि के सूत्रधार की तरह प्रेरणाप्रद नाट्यभंगिमा के साथ स्वयं कहता है:
‘इतिहास-पुरुष’ तीन भागों में विभक्त है। पहला भाग है, ‘परिचय’ जिसमें इतिहास-पुरुष नाटकीय गरिमा के साथ अपने स्वरूप का परिचय देता है। इस खण्ड में कवि ने निर्जीव यान्त्रिक कला-संचरण को विश्वात्मा का अमरत्व तथा जीवन चैतन्य का ऐश्वर्य प्रदान कर, उसके विभिन्न आयामों को अत्यन्त सशक्त एवं कलात्मक ढंग से चित्रित कर, लोकोत्तर चमत्कार पैदा कर दिया है। अपनी भूत-वर्तमान की उपलब्धियों तथा भावी सम्भावनाओं का उद्घाटन इतिहास-पुरुष जिस कवित्वपूर्ण राजसी ढंग से करता है, उसके गौरव से अभिभूत मन को सचमुच ही निष्कल निष्प्रपंच, क्रिया-गुणों से वर्जित अशरीरी ब्रह्म की कल्पना नीरस तथा निस्सार प्रतीत होने लगती है। निश्चय ही कवि ने अपनी अन्त:स्पर्शी प्रतिभा और विराट् ऋत कल्पना से अमूर्त ब्रह्म को इतिहास-पुरुष के रूप में लोकमंगलमय, जीवनमांसल रूप देकर, उसे सगुण, प्रगतिशील तथा भावमूर्त कर वैश्व सौन्दर्य से मण्डित कर दिया है। ऐसा लगता है कि शतियों की सौ करोड़ शाखाओं में बृहद् व्यापक इस विशाल वट पादप की स्वप्न मौन छाँह में खड़ा प्रबुद्धचेता रसवर्षी कवि विकासशील सृष्टि-तत्त्व का हस्तामलकवत् आर-पार निरीक्षण कर उसे जरारोगहीन अमर अनादि काल-विष्णु की गहरी नाभि-गुहा से निकले सहस्रनेत्र ब्रह्मकमल-स्वरूप इतिहास-पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है, जिसमें केवल दिक्सर्जित व्याप्ति ही नहीं, उद्बुद्ध लोक-जीवन की भावना-मनीषा में बहनेवाला अन्तर्लीन जाज्ज्वल्यमान तेज भी है। नि:सन्देह, इतिहास-पुरुष की चेतना से संयुक्त होकर ही मनुष्य जीवन तथा सृष्टि का अखण्ड प्रयोजन समझ सकता है, जैसा कि वह सृष्टि के सूत्रधार की तरह प्रेरणाप्रद नाट्यभंगिमा के साथ स्वयं कहता है:
पल में बदल देता मैं अपने ध्याता के
देह-प्राण, बुद्धि-मन,
और आँख-कान, और हो जाते प्रीति-घृणा,
और-और हास-रुदन
और-सी निगाहें, और दृष्टि, नयी भंगियाँ
......................
मेरे उपासकों के चित्त में समा जाते
नये अर्थबोध घने;
देह-प्राण, बुद्धि-मन,
और आँख-कान, और हो जाते प्रीति-घृणा,
और-और हास-रुदन
और-सी निगाहें, और दृष्टि, नयी भंगियाँ
......................
मेरे उपासकों के चित्त में समा जाते
नये अर्थबोध घने;
वह क्षुद्र लघु मानव की कुण्ठाग्रस्त,
काल-विषण्ण चेतना में नवीन जीवन-बोध का ज्वार उठाकर जैसे उसका सर्वांगीण
रूपान्तर कर देता है। इन प्रथम सात गीतों में डॉ. देवराज काल तथा जीवन की
अत्यन्त गम्भीर एवं जटिल सरणि को सर्वांगपूर्ण कलात्मक अभिव्यंजना देने
में सफल हुए हैं।
द्वितीय खण्ड में कवि जगत्-जीवन का ‘द्वन्द्वबोध’ देता है। यह खंड़ अत्यन्त प्राणवान्, सौन्दर्य-मांसल तथा जीवन-वैचित्र्यपूर्ण बन पड़ा है। कवि मानव से पूछता है कि वह इतने बड़े, ‘विविध वर्णगन्ध-भरे भूमि के पड़ावों में, देश-काल के शब्दित चौड़े फैलावों में’ आज अपने को क्यों उदास और अकेला अनुभव करता है ? वह अपनी शब्द-तूलि से जहाँ एक ओर धरती तथा मानव-जीवन के अनेक सौन्दर्य उल्लास-भरे चित्र उपस्थित करता है और इसी सिलसिले में ऋतुओं की बहार, ऊँचे शैल-शिखरों की शोभा-गरिमा, शैशव-यौवन की नयी पीढ़ियों की क्रीड़ा-किलोलें, स्त्री का आत्म-विस्मृत कर देनेवाला, अन्तस् में नये-नये भावबोध आँकनेवाला लावण्य, सिने-कलाकारों की नित्य नवीन भंगियाँ और योगियों के समान एकाग्रचित, सतत नये-नये प्रयोगों में निरत उदारमना वैज्ञानिकों का युगदान-रेडियो, वायुयानों की सुविधाओं आदि का-सौष्ठवपूर्ण वर्णन करता है, वहाँ दूसरी ओर मन्त्रियों, डिप्लोमेटों, राजदूतों, डायरेक्टरों आदि की रोबीली वेश-भूषा, सधी बातें, मँजी मुसकानें-आज के शुकपन्थी मार्क्स, सार्त्र, इलियट के भक्तों, बुद्धिजीवियों और आज की मूल्य-सूनी दुनिया में भय, संशय, नास्ति-भाव पीड़ित, तथ्यग्रस्त, वस्तुव्रती भौतिक सामाजिक शास्त्रों के अहम्मन्य पण्डितों की चर्चा कर युगजीवन की दयनीय विकृतियों पर भी निर्मम व्यंग्य प्रहार करने में नहीं चूकता। किन्तु इन सत्-असत्, सुन्दर-असुन्दर के द्वन्दों के भीतर क्रान्तदृष्टि कवि को मानव-जीवन की सार्थकता नहीं दिखाई देती। उसकी अन्तर्भेदिनी दृष्टि युगजीवन के इस धूल-धुन्ध के पार देखने की भी क्षमता रखती है। कवि के व्यापक दृष्टिकोण को वाणी देते हुए इतिहास-पुरूष कहता है
द्वितीय खण्ड में कवि जगत्-जीवन का ‘द्वन्द्वबोध’ देता है। यह खंड़ अत्यन्त प्राणवान्, सौन्दर्य-मांसल तथा जीवन-वैचित्र्यपूर्ण बन पड़ा है। कवि मानव से पूछता है कि वह इतने बड़े, ‘विविध वर्णगन्ध-भरे भूमि के पड़ावों में, देश-काल के शब्दित चौड़े फैलावों में’ आज अपने को क्यों उदास और अकेला अनुभव करता है ? वह अपनी शब्द-तूलि से जहाँ एक ओर धरती तथा मानव-जीवन के अनेक सौन्दर्य उल्लास-भरे चित्र उपस्थित करता है और इसी सिलसिले में ऋतुओं की बहार, ऊँचे शैल-शिखरों की शोभा-गरिमा, शैशव-यौवन की नयी पीढ़ियों की क्रीड़ा-किलोलें, स्त्री का आत्म-विस्मृत कर देनेवाला, अन्तस् में नये-नये भावबोध आँकनेवाला लावण्य, सिने-कलाकारों की नित्य नवीन भंगियाँ और योगियों के समान एकाग्रचित, सतत नये-नये प्रयोगों में निरत उदारमना वैज्ञानिकों का युगदान-रेडियो, वायुयानों की सुविधाओं आदि का-सौष्ठवपूर्ण वर्णन करता है, वहाँ दूसरी ओर मन्त्रियों, डिप्लोमेटों, राजदूतों, डायरेक्टरों आदि की रोबीली वेश-भूषा, सधी बातें, मँजी मुसकानें-आज के शुकपन्थी मार्क्स, सार्त्र, इलियट के भक्तों, बुद्धिजीवियों और आज की मूल्य-सूनी दुनिया में भय, संशय, नास्ति-भाव पीड़ित, तथ्यग्रस्त, वस्तुव्रती भौतिक सामाजिक शास्त्रों के अहम्मन्य पण्डितों की चर्चा कर युगजीवन की दयनीय विकृतियों पर भी निर्मम व्यंग्य प्रहार करने में नहीं चूकता। किन्तु इन सत्-असत्, सुन्दर-असुन्दर के द्वन्दों के भीतर क्रान्तदृष्टि कवि को मानव-जीवन की सार्थकता नहीं दिखाई देती। उसकी अन्तर्भेदिनी दृष्टि युगजीवन के इस धूल-धुन्ध के पार देखने की भी क्षमता रखती है। कवि के व्यापक दृष्टिकोण को वाणी देते हुए इतिहास-पुरूष कहता है
तेरी सब व्याधियों का
ओ मानव एकमात्र मैं ही निदान, भिषक्
मैं ही औषध तेरी,
मति तेरी, गति तेरी, धर्म कर्म सब तेरा....
....मेरी ही गोद में
तेरे मन-बुद्धि-अहम्
उगते पनपते हैं, उड़ते संकल्पों में
मेरे ही तेज़ क़दम;
ओ मानव एकमात्र मैं ही निदान, भिषक्
मैं ही औषध तेरी,
मति तेरी, गति तेरी, धर्म कर्म सब तेरा....
....मेरी ही गोद में
तेरे मन-बुद्धि-अहम्
उगते पनपते हैं, उड़ते संकल्पों में
मेरे ही तेज़ क़दम;
इसमें सन्देह नहीं कि इस बहुमुण्ड विभक्त
क्षणत्रस्त खण्ड जीवन की
सार्थकता तथा सत्यता हमें उसे इतिहास की पृष्ठभूमि के अखण्ड काल-प्रवाह से
संयुक्त करने ही से उपल होती है। नवीन भाव-गर्भित काव्यात्मक वाग्बन्धों
तथा रूपकों का सृजन करने में तथा नये-नये रूप-रंग-ध्वनियों की छटाओं का
सौन्दर्यदीप्त सम्मिश्रण करने में डॉ.देवराज की लेखनी ने सिद्धि प्राप्त
कर ली है। द्वन्द्व-बोध तथा जीवन के उत्थान-पतनों का चित्र उपस्थित करने
में कवि ने अनेक नवीन सुनहले बिम्बों, प्रतीकों द्वारा प्रभूत कवित्व,
शिल्प-सौन्दर्य तथा भावबोध बिखेरा है जिसकी ध्वनियाँ मन में निरन्तर
गूँजती रहती हैं।
‘प्रज्ञापारमिता’ शीर्षक अन्तिम खण्ड में युग-प्रबुद्ध जीवन-द्रष्टा कवि मनुष्य को नया प्रबोध देकर उसे इतिहास-पुरुष के अंक में एक ऐसे उच्च चैतन्य के धरातल पर खड़ा कर देता है जहाँ से वह समस्त सापेक्ष जगत्, जीवन की ऋजु कुंचित गतियों को तटस्थ, नि:संग, निरपेक्ष भाव से विराट् विश्व-चेतना में संयोजित देखकर विकास-क्रम को प्रगति देने के लिए उत्तरोत्तर नवीन प्रेरणाएँ ग्रहण कर सकने में समर्थ होता है। इस खण्ड का निर्माण कवि ने आत्मा के आलोक, मानस के परिमल पराग तथा प्राणों के प्रदीप्त पावक से किया है। क्षणजीवी मनुष्य में वह ऐसी अदम्य जिजीविषा तथा अखण्ड शक्ति भर देता है, जिसके अमृत संजीवन स्पर्श से वह कालचक्र के विपर्ययों के आघात से अविचलित रहकर सत्-असत्, ह्रास-विकास, हानि-लाभ की उद्धतफन, जिह्मगति तरंगों को चीरता हुआ आत्म-विश्वास, निष्ठा तथा निर्भीकता के साथ महज्जीवन के मंगलमय लक्ष्य की ओर अबाध गति से अग्रसर होने का बल प्राप्त करता है। मध्ययुगीन विराग, विरक्ति तथा वर्जना से मानव-चेतना को ऊपर उठाकर रसचेता कवि मनुष्य को उद्बुद्ध, रचना-प्रेमी, कर्मप्राण तथा अजेय आशावान् चैतन्य तथा जीवन-दृष्टि सौंप देता है। यह अन्तिम भाग अत्यन्त सशक्त, गम्भीर, कवित्वपूर्ण तथा जीवन के मंगल आलोक से ओतप्रोत है। इसमें डॉ. देवराज अत्यन्त समर्थ कवि के रूप में निखरे हैं। इतिहास के अकूल अतल समुद्र का मन्थन कर उन्होंने अपनी दर्शनज्ञ दृष्टि से जीवन-नवनीत स्वरूप जिस अक्षय तत्त्व को पाठकों के हाथों में रख दिया है, वह अपने आलोक, ऐश्वर्य, उपयोगिता तथा कवित्व में, चिरपुराण होते हुए भी, चिरनवीन अभिव्यक्ति के सौन्दर्य से आप्लावित है। शाश्वत के व्यापक अंक में युगजीवन जैसे अपनी अनेक अंग-भंगिमाओं में क्रीड़ा करता हुआ इस भावपंख काव्य में मूर्त हो उठा है। आदि से अन्त तक कवि का प्रेरणाप्रद उन्मेष ज्यों का त्यों बना ही नहीं रहता, वह अधिकाधिक विकसित तथा जीवन्त हो उठता है। कवि ने जिस नवीन काव्य-भाषा को जन्म दिया है वह अपनी सभी पिछली सीमाओं से मुक्त होकर नवीन युग-चेतना तथा भावबोध को सबल सौन्दर्यमयी अभिव्यक्ति देने में पूर्णरूपेण समर्थ हुई है। उसके अनेक शब्द-चित्र तथा वाक्य-बन्ध अक्षय सौन्दर्य कलशों की तरह अपना भावबोधगन्धी काव्यवैभव प्राणों में उँड़ेलते रहते हैं। अन्त में कवि के ही शब्दों में अखण्ड जीवन-चैतन्य के प्रति आस्था प्रकट करते हुए मैं इस स्वल्प प्राक्कथन को समाप्त करता हूँ-
‘प्रज्ञापारमिता’ शीर्षक अन्तिम खण्ड में युग-प्रबुद्ध जीवन-द्रष्टा कवि मनुष्य को नया प्रबोध देकर उसे इतिहास-पुरुष के अंक में एक ऐसे उच्च चैतन्य के धरातल पर खड़ा कर देता है जहाँ से वह समस्त सापेक्ष जगत्, जीवन की ऋजु कुंचित गतियों को तटस्थ, नि:संग, निरपेक्ष भाव से विराट् विश्व-चेतना में संयोजित देखकर विकास-क्रम को प्रगति देने के लिए उत्तरोत्तर नवीन प्रेरणाएँ ग्रहण कर सकने में समर्थ होता है। इस खण्ड का निर्माण कवि ने आत्मा के आलोक, मानस के परिमल पराग तथा प्राणों के प्रदीप्त पावक से किया है। क्षणजीवी मनुष्य में वह ऐसी अदम्य जिजीविषा तथा अखण्ड शक्ति भर देता है, जिसके अमृत संजीवन स्पर्श से वह कालचक्र के विपर्ययों के आघात से अविचलित रहकर सत्-असत्, ह्रास-विकास, हानि-लाभ की उद्धतफन, जिह्मगति तरंगों को चीरता हुआ आत्म-विश्वास, निष्ठा तथा निर्भीकता के साथ महज्जीवन के मंगलमय लक्ष्य की ओर अबाध गति से अग्रसर होने का बल प्राप्त करता है। मध्ययुगीन विराग, विरक्ति तथा वर्जना से मानव-चेतना को ऊपर उठाकर रसचेता कवि मनुष्य को उद्बुद्ध, रचना-प्रेमी, कर्मप्राण तथा अजेय आशावान् चैतन्य तथा जीवन-दृष्टि सौंप देता है। यह अन्तिम भाग अत्यन्त सशक्त, गम्भीर, कवित्वपूर्ण तथा जीवन के मंगल आलोक से ओतप्रोत है। इसमें डॉ. देवराज अत्यन्त समर्थ कवि के रूप में निखरे हैं। इतिहास के अकूल अतल समुद्र का मन्थन कर उन्होंने अपनी दर्शनज्ञ दृष्टि से जीवन-नवनीत स्वरूप जिस अक्षय तत्त्व को पाठकों के हाथों में रख दिया है, वह अपने आलोक, ऐश्वर्य, उपयोगिता तथा कवित्व में, चिरपुराण होते हुए भी, चिरनवीन अभिव्यक्ति के सौन्दर्य से आप्लावित है। शाश्वत के व्यापक अंक में युगजीवन जैसे अपनी अनेक अंग-भंगिमाओं में क्रीड़ा करता हुआ इस भावपंख काव्य में मूर्त हो उठा है। आदि से अन्त तक कवि का प्रेरणाप्रद उन्मेष ज्यों का त्यों बना ही नहीं रहता, वह अधिकाधिक विकसित तथा जीवन्त हो उठता है। कवि ने जिस नवीन काव्य-भाषा को जन्म दिया है वह अपनी सभी पिछली सीमाओं से मुक्त होकर नवीन युग-चेतना तथा भावबोध को सबल सौन्दर्यमयी अभिव्यक्ति देने में पूर्णरूपेण समर्थ हुई है। उसके अनेक शब्द-चित्र तथा वाक्य-बन्ध अक्षय सौन्दर्य कलशों की तरह अपना भावबोधगन्धी काव्यवैभव प्राणों में उँड़ेलते रहते हैं। अन्त में कवि के ही शब्दों में अखण्ड जीवन-चैतन्य के प्रति आस्था प्रकट करते हुए मैं इस स्वल्प प्राक्कथन को समाप्त करता हूँ-
हवा-नीर-माटी की अँधियारी खोहों में
ज्योतिवाही स्वर-अक्षर
जीवन-सन्देश लिये सदियों का आ रहे
सावधान स्वागत कर;
सावधान ! कवि, गायक, चिन्तक औ’ सन्त वे
मेरे आलोकप्राण,
रूपसुधा, रागसुरा, जीवन की श्रेय-सिद्धि
नित जिनसे स्यन्दमान;
जागृति-विवेक-बोध-मंगल के वारिवाह
रससोते प्रेरणा के
शुभ-सुन्दर चेतना के !
ज्योतिवाही स्वर-अक्षर
जीवन-सन्देश लिये सदियों का आ रहे
सावधान स्वागत कर;
सावधान ! कवि, गायक, चिन्तक औ’ सन्त वे
मेरे आलोकप्राण,
रूपसुधा, रागसुरा, जीवन की श्रेय-सिद्धि
नित जिनसे स्यन्दमान;
जागृति-विवेक-बोध-मंगल के वारिवाह
रससोते प्रेरणा के
शुभ-सुन्दर चेतना के !
सुमित्रानन्दन पन्त
परिचय
[1]
मैं हूँ इतिहास-पुरुष
भू की आक्षितिज जमी जड़ता की कीच से
शतदल-सा कढ़ा,
ग्रह-उपग्रह-तारों के जटित ज्योति-कक्षों की
छाया में बढ़ा;
सुरसरि के श्वेत-स्वच्छ लहरीले धारों के
ध्यान डूब धुला,
नील व्योमकुंजों के साँवरे रहस्यों की
राहों में खुला;
सत-रज-तम तीनों के रूप-गन्ध-रंग लिये
त्रिभुवन का लाड़ला
संसृति की चेतना-हिलोरों पर थिरक, खेल
मैं बढ़ता चला;
मेरी सौ लब्धियों के ध्वज-चिह्न सुरभीले
उभरे कुछ पत्र बड़े,
भावी सम्भावना-समूहों से शरमीले
बाक़ी सम्पुटित पड़े;
आदि-अन्त अनचीन्हे, वासना-भवरियों से
प्राण-क्रिया श्वेत-कलुष,
मैं हूँ इतिहास-पुरुष !
शतदल-सा कढ़ा,
ग्रह-उपग्रह-तारों के जटित ज्योति-कक्षों की
छाया में बढ़ा;
सुरसरि के श्वेत-स्वच्छ लहरीले धारों के
ध्यान डूब धुला,
नील व्योमकुंजों के साँवरे रहस्यों की
राहों में खुला;
सत-रज-तम तीनों के रूप-गन्ध-रंग लिये
त्रिभुवन का लाड़ला
संसृति की चेतना-हिलोरों पर थिरक, खेल
मैं बढ़ता चला;
मेरी सौ लब्धियों के ध्वज-चिह्न सुरभीले
उभरे कुछ पत्र बड़े,
भावी सम्भावना-समूहों से शरमीले
बाक़ी सम्पुटित पड़े;
आदि-अन्त अनचीन्हे, वासना-भवरियों से
प्राण-क्रिया श्वेत-कलुष,
मैं हूँ इतिहास-पुरुष !
[2]
जरा-रोगहीन अमर
मैं अनादि कालविष्णु की गहरी नाभिगुहा
से निकला ब्रह्मकमल,
सर्जन की गहन-गूढ़ उद्वेलित शक्तियों का
मैं ही हूँ केन्द्र प्रबल;
गन्धभरी हवा की तरंगों-सी फैल जातीं
मेरी अँगड़ाइयाँ,
वन-उपवन- बाग़ों पर छातीं बहार बन
मेरी परछाइयाँ;
मेरी स्मिति-रश्मियों का सोना बटोर-जोड़
बनती श्रीमन्त उषा,
चितवन की भंगिमाएँ बीन-सँजो तारकित
हो जाती सन्ध्या;
मेरी द्युतिछाया में नयी क्रान्ति, नया अर्थ
रवि- राशि- नक्षत्र वे
पा जाते; बस जाते जल-थल- भू- व्योम में
देवव्यूह कितने :
इन्द्र, वरुण, वह्नि, वात, पूषन्, पर्जन्य, उषा
अदिति, अर्यमा भास्वर
जरा-रोगहीन, अमर !
से निकला ब्रह्मकमल,
सर्जन की गहन-गूढ़ उद्वेलित शक्तियों का
मैं ही हूँ केन्द्र प्रबल;
गन्धभरी हवा की तरंगों-सी फैल जातीं
मेरी अँगड़ाइयाँ,
वन-उपवन- बाग़ों पर छातीं बहार बन
मेरी परछाइयाँ;
मेरी स्मिति-रश्मियों का सोना बटोर-जोड़
बनती श्रीमन्त उषा,
चितवन की भंगिमाएँ बीन-सँजो तारकित
हो जाती सन्ध्या;
मेरी द्युतिछाया में नयी क्रान्ति, नया अर्थ
रवि- राशि- नक्षत्र वे
पा जाते; बस जाते जल-थल- भू- व्योम में
देवव्यूह कितने :
इन्द्र, वरुण, वह्नि, वात, पूषन्, पर्जन्य, उषा
अदिति, अर्यमा भास्वर
जरा-रोगहीन, अमर !
[3]
व्यापक मैं हूँ विराट्
रोम-रोम में मेरे ज्ञान-क्रिया-भावाकुल
चित्तलोक बस रहे
बेगिनती; चेतना की स्वप्न-बोध-किरनों के
तार उलझ-फँस रहे;
मैं ही सहस्रनेत्र : लाख रूप-रंगों पर
दृग मेरे गड़ रहे,
मेरे हजार बाहु संसृति के कण-कण को
बरबस पकड़ रहे;
मेरी विशाल बुद्धि सूर्य-चन्द्र-तारों के
ताप- वेग नाप रही,
मेरी अतर्क्य शक्ति जल-थल, समीर-व्योम,
विद्युत को चाँप रही;
बलशाली आदिवाराह-सा प्रचण्ड मैं
भूतल का प्राणभार
ढो रहा, विश्व की तमिस्रा में ढाल रहा
प्रज्ञा की ज्योतिधार;
सपनों का स्वर्णलोक, आशा का ज्योतिक्षितिज
स्वयंकृती मैं स्वराट्
व्यापक मैं हूँ विराट् !
चित्तलोक बस रहे
बेगिनती; चेतना की स्वप्न-बोध-किरनों के
तार उलझ-फँस रहे;
मैं ही सहस्रनेत्र : लाख रूप-रंगों पर
दृग मेरे गड़ रहे,
मेरे हजार बाहु संसृति के कण-कण को
बरबस पकड़ रहे;
मेरी विशाल बुद्धि सूर्य-चन्द्र-तारों के
ताप- वेग नाप रही,
मेरी अतर्क्य शक्ति जल-थल, समीर-व्योम,
विद्युत को चाँप रही;
बलशाली आदिवाराह-सा प्रचण्ड मैं
भूतल का प्राणभार
ढो रहा, विश्व की तमिस्रा में ढाल रहा
प्रज्ञा की ज्योतिधार;
सपनों का स्वर्णलोक, आशा का ज्योतिक्षितिज
स्वयंकृती मैं स्वराट्
व्यापक मैं हूँ विराट् !
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i