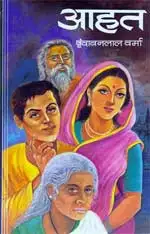|
विविध उपन्यास >> आहत आहतवृंदावनलाल वर्मा
|
415 पाठक हैं |
|||||||
बालक के साहस एवं लगन की अनूठी कथा....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
कहते हैं, यदि तीर लग जाए तो उसके घाव की पीड़ा कुछ समय में समाप्त हो
जाती है, किन्तु यदि बात लग जाए तो उसकी पीड़ा मन में हाहाकार मचा देती
है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी-कभी ऐसे निर्णय ले लेता है, जो उसे कहीं
से कहीं पहुँचा देते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में वर्माजी ने एक ऐसे ही बालक
के साहस एवं लगन की अनूठी कथा का वर्णन किया गया है।
परिचय
मैं तब साढ़े चार वर्ष का था। मऊरानीपुर
(जिला झाँसी) स्थित अपने घर के
सामने नंगा-उघाड़ा खेल रहा था। मेरे पिता से मिलने एक वृद्ध सज्जन आए।
मौलवी थे। इन्होंने मेरे पिता को छुटपन में उर्दू-फारसी पढ़ाई थी। इसका
चलन था। बिना इसकी जानकारी के सरकारी दफ्तरों में नौकरी नहीं मिल सकती थी।
मेरी कोई शरारत देखकर मौलवी साहब ने पूछा, ‘तुम्हारा बच्चा है ?’’
‘जी हाँ, इसे आप ही पढ़ा-लिखाकर दुनिया में खड़ा करेंगे।’
मुझे अपने पास प्यार से बुलाया गया। पिताजी ने मौलवी साहब से मुसकराते हुए कहा, ‘‘मांस आपका, हड्डी-हड्डी हमारी।’
यानी जब मौलवी साहब मुझे पढ़ाएँगे तब मेरी देह की वह सब दुर्गति होगी !
मैं सिकुड़कर रह गया और भागकर भीतर गया, माँ की गोद की शरण जा पकड़ी।
मैं उस सारे दृश्य को कभी नहीं भूला।
फिर जब मैं पाँच वर्ष का था, पिताजी झाँसी आ गए थे। एक दिन नंगा-धड़ंगा एक बछिया के पीछे दौड़धूप करता हुआ खेल रहा था कि पिताजी ने बुलाया। घर के चबूतरे पर एक वयोवृद्ध सज्जन हाथ में बेंत लिये खड़े थे।
पिताजी ने कहा, ‘आज से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी।’
मुझे मऊरानीपुरवाली बात याद आ गई-चबूतरे पर खड़े यह सज्जन अपने इसी बेंत से मेरी खाल-वाल उधेड़ेंगे ! भीतर गया। माता ने नहलाया-धुलाया, नई धोती पहनाई। सरस्वती-पूजन के बाद ‘पाटी-पूजन’ और ओम् नमः सिद्धम्’ हुआ, जिसे बुंदेलखंडी में ‘ओना मासीधम्’ कहते हैं। मिठाई खाने को मिली और माँ का प्यार। ‘हाड़-मांस’ वाली वह बात स्मृति के एक कोने में जा पड़ी।
फिर आठवीं कक्षा की पढ़ाई तक केवल एक बार बेंच पर खड़ा होना पड़ा था। घर में माता का प्यार और बाहर कई शिक्षकों का स्नेह पाता रहा। केवल एक बार पिताजी के कठोर बरताव पर घर से निकल भागने की ठानी और लगभग एक मील की दूरी तक नंगे पाँव चला भी गया था। मार्ग में काँटा लगा, माँ की याद आई और लौट आया। बाल्यावस्था की अनेक घटनाएँ आज भी याद हैं। उनका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे भी नहीं भूला हूँ। अन्य सहपाठियों और खेल के साथियों की भी बहुत सी बातें स्मृति में हैं।
सन् 1942 के लगभग मैं झाँसी म्यूनिसिपैलिटी (आज की नगरपालिका) की शिक्षा समिति का अध्यक्ष था। अंग्रेजी भी पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला गया। उसके प्रधान अध्यापक एम.ए., एल.टी. थे। एक दिन उनका आवेदन-पत्र मिला जिसमें लिखा था-‘एक बेंच की जरूरत है। खरीदने के लिए रुपए की स्वीकृति दी जावे।’
अध्यापकजी ने किस प्रयोजन से बेंत के लिए पैसे चाहे हैं, मैं समझ गया। मैंने स्वीकृति नहीं दी और उनसे ‘जवाब तलब’ किया-
‘यह बेंत किस उद्देश्य से आप लेना चाहते हैं ? क्या यह आपकी शिक्षा का माध्यम होगा ?’
अध्यापकजी पछताए और उन्होंने अपनी माँग वापस ले ली।
आज से तीन-चार वर्ष पहले मुझे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री आर.पी. कामठ की मित्रता उपलब्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने जीवन की अनेक घटनाएँ सुनाईं-छुटपन में घर से क्यों निकल भागे, बंबई में आकर एक भोजनालय में बरतन धोने तक का काम करते हुए कैसे अध्ययन करते रहे, और फिर वजीफा पाकर यूरोप में मूर्तिकला के सिद्धहस्त हुए।
हमारे जिले की भी कुछ घटनाएँ हैं-एक लड़का घर के बुरे बरताव के कारण निकल भागा। केवल माता का प्यार उसे प्राप्त था, परंतु वह अशक्त थी। लड़का उत्तर प्रदेश के एक बड़े नगर में पहुँचा और पढ़-लिखकर तैयार हो गया। फिर उसने अपने घर-द्वार को सँभाला। एक स्त्री ने सन् 1954 की बाढ़ में बुंदेलखंड की एक नदी में एक पड़ोसिन को डूबने से बचाते हुए अपने प्राण होम दिए थे। एक महाशय, यह बालक नहीं थे, होंगे लगभग चालीस के, घर की झंझट और फसाद से विकल होकर निकल भागे और अयोध्या की एक ‘साधु संगत’ में शामिल हो गए। घर में पत्नी और दो-तीन छोटे-छोटे बच्चे। इसमें एक होनहार था। अच्छा निकला। उसने अपने पुरवे में फैली हुई महामारी के दिनों में डटकर सेवाकार्य किया। कई लोगों के प्राण बच गए। समाचार एक पत्र में प्रकाशित हुआ उन ‘साधु’ सज्जन ने भी पढ़ा। वह उस ‘संगत’ से विरक्त होकर अपने घर लौट आए और सुधरा हुआ जीवन बिताने लगे। उन्हें अपने पुत्र का अभिमान था। ‘उतनी दूरी से इसी ने मुझे मटरगश्ती से बचाया,’ कहा करते थे।
इस उपन्यास में ऊपर की अनेक बातों का समन्वय किया गया है, और दहेज प्रथा का घोर विरोधी तो मैं सदा ही रहा हूँ। उपन्यास की दलेजवाली घटना पाँच-छह वर्ष पहले की है। समाचार-पत्रों में पूरा विवरण प्रकाशित हुआ था। उस स्थान का नाम नहीं बतलाऊँ गा। जहाँ वे घटनाएँ घटी थीं। यह सब उपन्यास में समन्वित कर दिया गया है।
कुल घटनाएँ तथ्यों पर आधारित हैं। मैं बाल मनोविज्ञान का भी विद्यार्थी हूँ। बालकों के साथ, उनके छुटपन से ही, कैसा बरताव करना चाहिए और जिन बालकों में कुछ समझ आ गई है उन्हें किस प्रकार आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, इसकी जानकारी की बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रेरणा से कहानी का साधन अपनाकर यह उपन्यास लिखा है।
जिन दिनों इस उपन्यास के लिखने की सोच रहा था, बतखों और कुत्तेवाली घटना का विवरण पढ़ा-बतखों ने अपने मित्र, एक कुत्ते को दूसरे से बचाया था, जो उसका शत्रु था। हम मानव भी एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं और अधिक क्यों न करें ?
मेरी कोई शरारत देखकर मौलवी साहब ने पूछा, ‘तुम्हारा बच्चा है ?’’
‘जी हाँ, इसे आप ही पढ़ा-लिखाकर दुनिया में खड़ा करेंगे।’
मुझे अपने पास प्यार से बुलाया गया। पिताजी ने मौलवी साहब से मुसकराते हुए कहा, ‘‘मांस आपका, हड्डी-हड्डी हमारी।’
यानी जब मौलवी साहब मुझे पढ़ाएँगे तब मेरी देह की वह सब दुर्गति होगी !
मैं सिकुड़कर रह गया और भागकर भीतर गया, माँ की गोद की शरण जा पकड़ी।
मैं उस सारे दृश्य को कभी नहीं भूला।
फिर जब मैं पाँच वर्ष का था, पिताजी झाँसी आ गए थे। एक दिन नंगा-धड़ंगा एक बछिया के पीछे दौड़धूप करता हुआ खेल रहा था कि पिताजी ने बुलाया। घर के चबूतरे पर एक वयोवृद्ध सज्जन हाथ में बेंत लिये खड़े थे।
पिताजी ने कहा, ‘आज से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी।’
मुझे मऊरानीपुरवाली बात याद आ गई-चबूतरे पर खड़े यह सज्जन अपने इसी बेंत से मेरी खाल-वाल उधेड़ेंगे ! भीतर गया। माता ने नहलाया-धुलाया, नई धोती पहनाई। सरस्वती-पूजन के बाद ‘पाटी-पूजन’ और ओम् नमः सिद्धम्’ हुआ, जिसे बुंदेलखंडी में ‘ओना मासीधम्’ कहते हैं। मिठाई खाने को मिली और माँ का प्यार। ‘हाड़-मांस’ वाली वह बात स्मृति के एक कोने में जा पड़ी।
फिर आठवीं कक्षा की पढ़ाई तक केवल एक बार बेंच पर खड़ा होना पड़ा था। घर में माता का प्यार और बाहर कई शिक्षकों का स्नेह पाता रहा। केवल एक बार पिताजी के कठोर बरताव पर घर से निकल भागने की ठानी और लगभग एक मील की दूरी तक नंगे पाँव चला भी गया था। मार्ग में काँटा लगा, माँ की याद आई और लौट आया। बाल्यावस्था की अनेक घटनाएँ आज भी याद हैं। उनका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे भी नहीं भूला हूँ। अन्य सहपाठियों और खेल के साथियों की भी बहुत सी बातें स्मृति में हैं।
सन् 1942 के लगभग मैं झाँसी म्यूनिसिपैलिटी (आज की नगरपालिका) की शिक्षा समिति का अध्यक्ष था। अंग्रेजी भी पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला गया। उसके प्रधान अध्यापक एम.ए., एल.टी. थे। एक दिन उनका आवेदन-पत्र मिला जिसमें लिखा था-‘एक बेंच की जरूरत है। खरीदने के लिए रुपए की स्वीकृति दी जावे।’
अध्यापकजी ने किस प्रयोजन से बेंत के लिए पैसे चाहे हैं, मैं समझ गया। मैंने स्वीकृति नहीं दी और उनसे ‘जवाब तलब’ किया-
‘यह बेंत किस उद्देश्य से आप लेना चाहते हैं ? क्या यह आपकी शिक्षा का माध्यम होगा ?’
अध्यापकजी पछताए और उन्होंने अपनी माँग वापस ले ली।
आज से तीन-चार वर्ष पहले मुझे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री आर.पी. कामठ की मित्रता उपलब्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने जीवन की अनेक घटनाएँ सुनाईं-छुटपन में घर से क्यों निकल भागे, बंबई में आकर एक भोजनालय में बरतन धोने तक का काम करते हुए कैसे अध्ययन करते रहे, और फिर वजीफा पाकर यूरोप में मूर्तिकला के सिद्धहस्त हुए।
हमारे जिले की भी कुछ घटनाएँ हैं-एक लड़का घर के बुरे बरताव के कारण निकल भागा। केवल माता का प्यार उसे प्राप्त था, परंतु वह अशक्त थी। लड़का उत्तर प्रदेश के एक बड़े नगर में पहुँचा और पढ़-लिखकर तैयार हो गया। फिर उसने अपने घर-द्वार को सँभाला। एक स्त्री ने सन् 1954 की बाढ़ में बुंदेलखंड की एक नदी में एक पड़ोसिन को डूबने से बचाते हुए अपने प्राण होम दिए थे। एक महाशय, यह बालक नहीं थे, होंगे लगभग चालीस के, घर की झंझट और फसाद से विकल होकर निकल भागे और अयोध्या की एक ‘साधु संगत’ में शामिल हो गए। घर में पत्नी और दो-तीन छोटे-छोटे बच्चे। इसमें एक होनहार था। अच्छा निकला। उसने अपने पुरवे में फैली हुई महामारी के दिनों में डटकर सेवाकार्य किया। कई लोगों के प्राण बच गए। समाचार एक पत्र में प्रकाशित हुआ उन ‘साधु’ सज्जन ने भी पढ़ा। वह उस ‘संगत’ से विरक्त होकर अपने घर लौट आए और सुधरा हुआ जीवन बिताने लगे। उन्हें अपने पुत्र का अभिमान था। ‘उतनी दूरी से इसी ने मुझे मटरगश्ती से बचाया,’ कहा करते थे।
इस उपन्यास में ऊपर की अनेक बातों का समन्वय किया गया है, और दहेज प्रथा का घोर विरोधी तो मैं सदा ही रहा हूँ। उपन्यास की दलेजवाली घटना पाँच-छह वर्ष पहले की है। समाचार-पत्रों में पूरा विवरण प्रकाशित हुआ था। उस स्थान का नाम नहीं बतलाऊँ गा। जहाँ वे घटनाएँ घटी थीं। यह सब उपन्यास में समन्वित कर दिया गया है।
कुल घटनाएँ तथ्यों पर आधारित हैं। मैं बाल मनोविज्ञान का भी विद्यार्थी हूँ। बालकों के साथ, उनके छुटपन से ही, कैसा बरताव करना चाहिए और जिन बालकों में कुछ समझ आ गई है उन्हें किस प्रकार आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, इसकी जानकारी की बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रेरणा से कहानी का साधन अपनाकर यह उपन्यास लिखा है।
जिन दिनों इस उपन्यास के लिखने की सोच रहा था, बतखों और कुत्तेवाली घटना का विवरण पढ़ा-बतखों ने अपने मित्र, एक कुत्ते को दूसरे से बचाया था, जो उसका शत्रु था। हम मानव भी एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं और अधिक क्यों न करें ?
झाँसी
28.9.1960
28.9.1960
-वृंदावनलाल वर्मा
आहत
:1:
‘क्यों रे, मानता नहीं ! आऊँ मैं ?
पढ़े न लिखे, ऊधम-ही-ऊधम
करता रहता है।’ मंजरी रसोईघर में से चिल्लाई।
‘यों ही लगी हो, माँ, तुम तो। इन चिड़ियों की चाँय-चाँय के मारे पढ़ना दूभर हो रहा है; बीट कर-कर दे रही हैं, लिखूँ कैसे ?’ आठ बरस के दीपसिंह ने प्रतिवाद किया। उसके स्वर में कुछ रुआँसापन था। तीखापन बिल्कुल नहीं। परंतु उसने आँखें इस तरह मीचीं-मटकाईं कि यदि उसे कोई देख रहा होता तो समझ लेता कि रुआँसापन केवल बनावट है।’
मंजरी उसकी माँ थी। रसोईघर में खाना बना रही थी।
कार्तिक का महीना था। दिन चढ़ आया था। अमरपुर गाँव के नीचे होकर बहनेवाली डुमरई नाम की नदी की दिशा से पवन की ठंडी झकोर आ-आकर दीपसिंह को और आँगन में खड़े उस नीम के पेड़ को मौज दे रही थी, जिसके नीचे वह बैठा था। दीपसिंह के सामने उसका बस्ता था, जिसे मंजरी रसोई का कार्यारंभ करने के पहले पढ़ने को ताकीद करके सामने रखवा गई थी।
टाट के मैले से बोरे पर दीपसिंह बस्ता फैलाकर थोड़ी ही देर बैठा था कि आँगन के एक कोने में दीवार की खूँटी से टँगी गुलेल पर उसकी आँख दौड़ी। फिर पेड़ की डालों पर चहकनेवाली चिड़ियों पर। घर का आँगन लंबा-चौड़ा था, नीम का पेड़ पुराना। पेड़ के मोटे तने पर दीमक की लाई मिट्टी जगह-जगह चढ़ी हुई थी। एक मोटी डाल के जोड़ का बड़ा भाग खोखला हो चुका था। कुछ डालें हरिया रही थीं, कुछ की पत्तियाँ खिरबिर्री हो गई थीं। सूरज की सुनहली किरणों में पत्तियाँ थिरक-थिरककर दमक रही थीं, मानों चिड़ियों की चहक पर झूम रही हों। आँगन का रसोई की ओरवाला भाग लिपा हुआ था। एक बड़े भाग में कंकड़ कहीं गड़े, कहीं बिखरे पड़े थे। वहाँ अभी धूप नहीं आई थी।
दीपसिंह की आँखें कुछ ढूँढ़ने लगीं। बाँस, के एक टुकड़े पर जा अटकीं। तुरंत उठा और उसने उस टुकड़े से गुलेल नीचे गिरा ली। चिड़ियाँ आने-जाने लगीं। उसने कुछ कंकड़ बीनकर बस्ते पर रख लिये और उड़ते-बैठते पक्षियों पर गुलेल से कंकड़ फटकारने लगा।
गुलेल उसके पिता ने साइकिल की पुरानी ट्यूब के टुकड़े से बनाई थी। दीपसिंह बराबर गुलेल चलाता रहा, कंकड़ लगा एक चिड़िया के भी नहीं। नीम की छोटी-छोटी टहनियों से पत्तियाँ जरूर झड़-झड़कर गिर रही थीं।
उस बड़े आँगन के चारों तरफ छोटे-बड़े कमरे थे। केवल एक कोने पर टूटी हुई दीवार थी और पुराने चूने के छोटे-छोटे ढोंके उसके नीचे इधर-उधर पड़े थे। यह टूटी हुई दीवार दो-तीन हाथ ऊँची होगी। इसके नीचे होकर आँगन के पानी का बहाव था और बाहर लगा हुआ नाबदान। नाबदान एक बड़े से खंडहर में था। उस खंडहर में झाड़ी-झंखाड़ था, जहाँ होकर कम-से-कम गाँव के जानवर तो आँगन में नहीं आ सकते थे।
चिड़ियाँ चहचहाहट करती हुई टूटी दीवार के बाहरवाले झाड़ों पर कुदकने-फुदकने लगीं। दीपू ने उधर भी कंकड़ सन्नाए। चिड़ियाँ वहाँ से उड़कर आँगन के कमरों की खपरौल पर चीं-चीं कर उठीं। वहीं बगल में खपरैलवाला रसोईघर था। चिड़ियाँ उस पर पहुँचने से क्यों चूँकतीं ! दीपसिंह ने उस ओर भी कंकड़ फेंके। रसोईघर के छप्पर पर गिरे। उसकी माँ आँगन में निकल आई।
मंजरी की आयु छब्बीस-सत्ताईस के लगभग होगी। बड़ी-बड़ी आखोंवाली गोरी-साँवली; छरेरी सुंदर आकृति की थी। बहुत स्वस्थ थी। माथे पर कार्तिक स्नान की चंदन-खौर को आतंकमय बनाने का प्रयत्न करने पर भी मंजरी को डरावना न बना सकी। चिल्लाई, ‘टाट पर बस्ता खुला पड़ा है, चिड़ियों के पीछे पकड़कर आँगन भर में कंकड़ बिखेर रहा है ! पढ़ता क्यों नहीं रे ?’
‘कापी-किताबों पर चिड़ियों ने बीट कर दी तो ? फिर इतना हल्ला कर रही हैं कि पढ़ नहीं पाता हूँ।’ दीपू ने मुँह बिगाड़कर कहा।
‘कितने हरे-हरे पत्तें गिरा दिए तूने ! क्यों सत्यानास पर तुला है ?’
‘यह लो ! दातूनें तोड़ती हो तब तो ढेर सारे पत्ते गिर जाते हैं।’
‘आने दे उन्हें, तेरी मरम्मत कराऊँगी।’
‘लो, मैं पढ़ता तो हूँ। वैसे ही लगी हो। वह देखो, चिड़ियाँ रसोईघर के खपरों को गंदा कर रही हैं।’
दीपसिंह गुलेल एक तरफ रखकर बस्ते के पास बैठ गया और पढ़ने-लिखने की सामग्री इधर-उधर करने लगा। मंजरी रसोईघर में चली गई। दीपसिंह ने सोचा, गुलेल जहाँ की तहाँ टाँग दूँ। थोड़ा सा प्रयत्न करने पर सफल हो गया। कुछ ही क्षण पीछे चिड़ियाँ फिर चाँय-चाँय करती हुई नीम पर आने-जाने लगीं। उसने आसपास से कंकड़ उठा-उठाकर चिड़ियों को फेंकने शुरू किए; परंतु रसोईघर की दिशा में नहीं चलाए।
उसका पिता कहीं गाँव में गया था, जिसका भय मंजरी उस धमकी में छोड़ गई थी। सामने पौर थी। आहट मिली, जैसे कोई आ रहा हो। दीपू ने तुरंत एक पुस्तक खोलकर इस प्रकार हाथ में ली जैसे बड़ी लगन के साथ पढ़ रहा हो।
आनेवाले ने पौर से ही पुकारा, ‘मालिक हैं ?’
दीपसिंह ने पुस्तक अलग रख दी। बोला, ‘कौन है ?’
आगंतुक आँगन में आ गया।
‘क्या है, दमरू ?’ दीपसिंह ने पूछा।
दमरू अधेड़ अवस्था का दुबला सा व्यक्ति था। स्वास्थ्य उससे कभी का विदा ले चुका होगा। चेहरे पर शिकनें थीं। फटे साफे के नीचे से अधभूरे बाल झाँक रहे थे। ठोड़ी पर उसी रंग की दस-बीस दिन की हजामत होगी।
‘मालिक हैं, भैया सा’ब ?’ उसने प्रश्न दुहराया।
‘क्यों ?’
‘तिल्ली की झार-फूँक करवानी है। आज बुधवार है न।’
‘वह तो कहीं गाँव में देर के निकल गए हैं। बैठ जाओ, आते ही होंगे।’
दमरू आँगन की पौरवाली दीवार से सटकर बैठ गया। दीपू ने पढ़ना-लिखना शुरू ही नहीं किया था, बातें करने लगा, ‘कब से है तुम्हें तिल्ली ?’
‘न जाने कब से है, भैया। अब बढ़ गई है।’
‘कोई दवा खाई ?’
‘बहुत सी खा लीं, कुछ नहीं हुआ। अब तो दवा के लिए पैसा ही गाँठ में नहीं है।’
‘झारा-फूँकी से जरूर फायदा होगा। हमारे पिताजी बात-की-बात में छू कर देंगे।’
‘इसलिए तो आया हूँ, भैया सा‘ब’।
मंजरी चौके से फिर निकल आई। बोली, ‘पहले नीम की डालें तोड़ रहा था, अब बातें मठोल रहा है। पढ़ने-लिखने से तो तूने बैर कर रक्खा है।’
दीपू ने बात बनाई, ‘पढ़ तो रहा था, बिलकुल पढ़ रहा था। इतने में दादा को यह दमरू पूछते आ गए।’
दीपू ने एक पुस्तक खोल ली, जैसे पढ़ने के लिए तल्लीन होने वाला हो। धीरे-धीरे मरमराता रहा, ‘नीम की मैंने कौन सी डाल तोड़ी है ! उँह !’
मंजरी ने कुछ रुलाई के साथ दमरू से कहा, ‘गाँव में ढूँढ़ लो उन्हें। या बैठना हो तो पौर में जा बैठो, लड़के से बात न करो, पढ़ रहा है।’
दमरू खाँसता-साँस भरता चला गया। मंजरी रसोईघर में लौट गई। दीपसिंह ने पुस्तक बंद कर दी और एक कॉपी पर कुछ रेखाएँ खींचने-बनाने लगा।
दमरू पौर में नहीं बैठा, बाहर निकल गया। तिल्ली या किसी बीमारी से बढ़कर उसे चिंता अपने काम-मजूरी की थी। आज बुधवार को झाड़ा-फूँकी न करवा पाई तो अगले रविवार के दिन देखा जावेगा-सोचता जा रहा था कि पड़ोस में लुहार की दूकान से एक गूँज कान में पड़ी।
लुहार की दूकान उस घर से थोड़ी ही दूर पर थी। जरा चले, एक गली में मुड़े कि नत्थू लुहार की दूकान। दमरू दरवाजे से झाँककर आड़ में खड़ा हो गया। ‘राम-राम, मालिक’ कहकर अदब की आँखों दूकान के भीतर दृष्टि फेरने लगा। एक तरफ चढ़ी अवस्था का तगड़ा लुहार ऊँची-चौड़ी निहानी पर हथौड़े से खुरपी-हँसिए पीट रहा था। धौंकनी एक बुढ़िया चला रही थी। जब नत्थू भट्ठी में से औजार निकालता तभी बुढ़िया का हाथ रुकता था। दूसरी ओर काठ की छोटी सी तिपाई पर बैठा अंगद बीड़ी पी रहा था, जिसे दमरू ने ‘राम-राम, मालिक’ की थी; जिसके उत्तर में उसने केवल जरा सा सिर हिलाया था। अंगद की आँखें मदीली थीं, रसभरी-सी बड़ी-बड़ी। गोरे चेहरे पर चेचक के दागों में एकाध रेखा आ बैठी थी। आयु वैसे अधिक न होगी, वही कोई तीस-बत्तीस साल की। हथौड़े की चोटों और बीड़ी की फूँकों के बीच बातें चल रही थीं।
नत्थू ने कहा, ‘अखबारों में तो बड़ी गरम खबरें छपने लगी हैं। सुनते हैं कि....’
अंगद ने बात काटकर समाधान किया, ‘अरे मिस्त्री, अखबारी टप्पे हैं। देश के एक-तिहाई में तो रियासतें ही हैं, बाकी को जमींदार पाटे हुए हैं। भगवान् ने जमींदार और राजा मिटने के लिए नहीं बनाए हैं।’
नत्थू की थोड़ी सी भूमि थी और उसकी दूकान पर अधिकांश किसान ही आया करते थे। समाचार-पत्रों में छपी बातें घूमती-फिरती उसके यहाँ भी आ जाती थीं। किसान भी मिटने के लिए नहीं बनाए गए हैं, उसके मन में उठा। बोला, ‘मिटता कोई नहीं है।’
अंगद ने उसे बीड़ी दी, काम बंद हुआ। प्रसंग चलता रहा।
नत्थू कहता रहा, ‘हाँ-आँ, जो कुछ इतने जुगों से चला आ रहा है, फूँक मारने से तो मिटता नहीं। पर भगवान् की माया विचित्र है, पहाड़ का तिल और तिल का पहाड़ वे ही कर देते हैं। आदमी बिचारा क्या कर सकता है ?’
अगंद अपनी धुन में था-
‘रईसों के पुरखों ने रियासतें और हमारे पुरखों ने भूमि रक्त की नदियाँ बहाकर कमाई हैं। ऐसे ही नहीं मिट सकतीं।’ हलकी सी हँसी से उसने अपना तर्क चिकना कर लिया।
नत्थू बहस नहीं करना चाहता था, उसे अभ्यास ही न था। पर उसने इससे कुछ उलटा सुन रखा था, कुछ देखा भी था। कहा, ‘भगवान् जो चाहते हैं वही होता है।’ और वह फिर हथौड़ा चलाने लगा।
अंगद मझोले दरजे का जमींदार था। पचास एकड़ के लगभग होगी उसकी भूमि। समझता अपने को जरा बड़ा था, ऊँची जाति का था ही। दमरू ने वहीं से हाथ जोड़कर उसे अपनी ओर आकृष्ट किया।
‘क्या है, दमरू ?’ अंगद ने बिना किसी रुचि के पूछा।
दमरू ने गिड़गिड़ाकर कहा, ‘आज बुधवार है, मालिक, झड़वाने् आया हूँ।’
अंगद की उन मदीली आँखों में दर्प और दंभ दोनों आ गए, ‘सो यह समय है झाड़ा-फूँकी का ! बड़े भोर आना चाहिए था।’
नत्थू हाथ रोककर बोला, ‘न जाने कितने गरीब निहाल हो गए हैं आपके हाथ से। कर दीजिए बिचारे का भला।’
उस गरीब से अधिक उस क्षण नत्थू अपना भला करना चाहता था, जमींदार जी चले जाएँ तो अपना काम बेखटके करता रहूँ।
‘हाँ, मालिक, बड़ा जस है आपके हाथ में।’ दमरू ने निवेदन किया।
अंगद साँप काटे की, तिल्ली की और न जाने कितने मर्जों की झाड़ा-फूँकी किया करता था। इधर-उधर की जड़ी-बूटियाँ भी कभी-कभी प्रयोग में लाता था। कुछ अच्छे हो गए, कुछ मर गए। जो अच्छे हो गए थे वे उसके करतब से, जो मर गए वे अपने भाग्य से।
बीड़ी का अंतिम टुकड़ा, जिसमें तंबाकू का एकाध कण मात्र रह गया होगा, फेंककर अंगद मूँछों पर हाथ फेरता हुआ कुछ सोचने लगा।
‘अच्छा, चलो घर।’ अंगद ने दमरू से कहा और दूकान से बाहर निकल आया। दमरू उसके पीछे हो लिया।
पौर में पहुँचकर दमरू से अप्रत्याशित कोमल स्वर में बोला, ‘यहीं बैठ जाओ, मैं हाथ-पाँव धोकर आता हूँ।’
दमरू बैठ गया। कितने अच्छे हैं मालिक, उसने सोचा।
अंगद ने आँगन में जाकर हाथ-पाँव धोए।
आहट पाकर मंजरी रसोईघर से निकल आई। मुसकराकर बोली, ‘कलेवा कर लो।’
दीपसिंह, जो अभी कॉपी पर रेखाएँ खींच रहा था, बोला, ‘दमरू तिल्ली का रोग झड़वाने आया है, वह कब तक बैठा रहेगा ?’
‘ओ हो ! सारे जग की चिंता है न तुझे !’ मंजरी के स्वर में मिठास थी।
‘तुमने कलेवा कर लिया, बेटा ?’ अंगद ने पूछा।
‘नहीं तो, भोर से लिखने-पढ़ने में जो लगा हूँ।’ दीपू ने उत्तर दिया।
‘हाँ-हाँ, बड़ा पढ़नेवाला है ! तभी से गुलेल चला रहा है यह !’ मंजरी के होंठों पर मुसकान थी।
कॉपी पर आँख घुमाते हुए अंगद ने दीपू को शाबाशी दी, ‘कॉपी पर आर्ट बना रहा है, जिसे लोग कला कहते हैं। किसी दिन बड़ा कलाकार होगा दीप।’
‘अहा हा-हा ! जरूर होगा। ऐसे ही बिगाड़े जाओ इसे।’ मंजरी की भर्त्सना में खीज जरा भी न थी। उसने अंगद से कलेवा करने का फिर अनुरोध किया।
‘दमरुआ का मंत्र-जंत्र करके अभी आता हूँ। तब तक तुम कलेवा कर लो, बेटा। स्कूल का समय भी होने को है। हाथ-पाँव धो लिये हैं; पहले यह काम कर लूँ।’ कहकर अंगद पौर में चला गया।
दीपू का चाहे मन लग रहा हो, चाहे दिखलावे के लिए हो, वह कॉपी पर कला की रेखाएँ बनाता रहा।
अंगद ने झाड़ा-फूँकी के बाद दमरू को कुछ परहेज बतलाकर बातचीत की, ‘आज काम पर कहाँ जाना है ?’
दमरू के पास निज का कोई खेत न था। जिसके यहाँ मजूरी पर जाना था। उसका नाम बतला दिया।
‘हमारे यहाँ करोगे काम सोंझ-बटाई पर ?’ जैसे ही अंगद से पूछा, दमरू ने धरती पर सिर टेककर हामी भरी और हाथ जोड़कर बैठ गया।
अंगद ने सोंझ की शर्ते बतलाईं, ‘एक हिस्सा तुम्हारा और तीन हमारे। हमारी भूमि बहुत बढ़िया है। बैल-बीज वगैरह भी हमारे रहेंगे, तुम्हें तो खेत बनाने भर हैं। आजकर उसमें पानी भरा है। धीरे-धीरे सूख रहा है। बखरकर बीज बोना भर है। थोड़ी सी निदाई, रखवाली वगैरह। सो तुम सब जानते ही हो।’
दोनों तरह की ‘वगैरह’ में जो कुछ लुका-छिपा था उसे दमरू जानता था, तो भी अंगद ने थोड़ा सा ब्योरा दिया।
दमरू अब भी हाथ जोड़े बैठा था।
‘जमीन का लगान, मालगुजारी और बीज की सवाई काटकर गल्ला और भूसा बाँट लिया जाएगा। कटाई तुम्हारे जिम्मे रहेगी, खलिहान का काम-धाम तो खैर करोगे ही।’
दमरू के जुड़े हुए हाथ कुछ ढीले पड़ गए। फिर भी उसने हामी भरी और नम्रता के साथ अपनी एक कठिनाई पेश की, ‘मालिक, फसल आने तक हमारे खाने के लिए ?’
दमरू के स्वर में अंगद को कुछ निर्बलता भासित हुई।
‘हम देंगे। वाह ! भूखों थोड़ी मरने देंगे। जैसे ही फसल कटने पर अनाज गाहा, तुम्हारे हिस्से में से इन दिनों की खवाई सवाई समेत काट लेंगे। कायदा है न !’
‘सवाई समेत, मालिक ?’
‘अच्छा भई, सवाई नहीं, रुपए के अठारह आना, बस ?’
दमरू ने हामी भरी।
भीतर से कलेवा करने का तकाजा फिर हुआ।
‘मैं तुम्हारी तिल्ली को ठीक करके रहूँगा। बैठना, तुम्हारे लिए भी कलेवा आता है।’ आश्वासन देकर अंगद भीतर चला गया।
पराँठे बने थे। अंगद कलेवा करने लगा। चेहरे पर प्रसन्नता की लहर थी।
मंजरी ने कहा, ‘कार्तिक की पूनो आ रही है।’
‘हाँ-हाँ, हर साल कार्तिक नहाती हो और पूनो आती है।’
‘इस साल जरा अच्छी सी साड़ी आनी चाहिए।’
‘जरूर आएगी,’ अंगद ने मुसकराते हुए भरोसा दिया।
मंजरी ने दीपू को बुलाया और उसके हाथ में दमरू के लिए बासी रोटियाँ दे दीं। दीपू ने अपने लिए भी कलेवा लिया और साथ में आम का अचार। पौर में जाकर उसने रोटियों के साथ दमरू को अपने कलेवे में से एक पराँठा और आम का अचार दे दिया। फिर आंगन में जाकर बचे हुए पराँठे चल-फिरकर धीरे-धीरे खाने लगा। बस्ता बिखरा पड़ा था। चिड़ियाँ चहक-चहककर उड़ रही थीं। उसे स्कूल पहुँचने की जल्दी न थी।
‘यों ही लगी हो, माँ, तुम तो। इन चिड़ियों की चाँय-चाँय के मारे पढ़ना दूभर हो रहा है; बीट कर-कर दे रही हैं, लिखूँ कैसे ?’ आठ बरस के दीपसिंह ने प्रतिवाद किया। उसके स्वर में कुछ रुआँसापन था। तीखापन बिल्कुल नहीं। परंतु उसने आँखें इस तरह मीचीं-मटकाईं कि यदि उसे कोई देख रहा होता तो समझ लेता कि रुआँसापन केवल बनावट है।’
मंजरी उसकी माँ थी। रसोईघर में खाना बना रही थी।
कार्तिक का महीना था। दिन चढ़ आया था। अमरपुर गाँव के नीचे होकर बहनेवाली डुमरई नाम की नदी की दिशा से पवन की ठंडी झकोर आ-आकर दीपसिंह को और आँगन में खड़े उस नीम के पेड़ को मौज दे रही थी, जिसके नीचे वह बैठा था। दीपसिंह के सामने उसका बस्ता था, जिसे मंजरी रसोई का कार्यारंभ करने के पहले पढ़ने को ताकीद करके सामने रखवा गई थी।
टाट के मैले से बोरे पर दीपसिंह बस्ता फैलाकर थोड़ी ही देर बैठा था कि आँगन के एक कोने में दीवार की खूँटी से टँगी गुलेल पर उसकी आँख दौड़ी। फिर पेड़ की डालों पर चहकनेवाली चिड़ियों पर। घर का आँगन लंबा-चौड़ा था, नीम का पेड़ पुराना। पेड़ के मोटे तने पर दीमक की लाई मिट्टी जगह-जगह चढ़ी हुई थी। एक मोटी डाल के जोड़ का बड़ा भाग खोखला हो चुका था। कुछ डालें हरिया रही थीं, कुछ की पत्तियाँ खिरबिर्री हो गई थीं। सूरज की सुनहली किरणों में पत्तियाँ थिरक-थिरककर दमक रही थीं, मानों चिड़ियों की चहक पर झूम रही हों। आँगन का रसोई की ओरवाला भाग लिपा हुआ था। एक बड़े भाग में कंकड़ कहीं गड़े, कहीं बिखरे पड़े थे। वहाँ अभी धूप नहीं आई थी।
दीपसिंह की आँखें कुछ ढूँढ़ने लगीं। बाँस, के एक टुकड़े पर जा अटकीं। तुरंत उठा और उसने उस टुकड़े से गुलेल नीचे गिरा ली। चिड़ियाँ आने-जाने लगीं। उसने कुछ कंकड़ बीनकर बस्ते पर रख लिये और उड़ते-बैठते पक्षियों पर गुलेल से कंकड़ फटकारने लगा।
गुलेल उसके पिता ने साइकिल की पुरानी ट्यूब के टुकड़े से बनाई थी। दीपसिंह बराबर गुलेल चलाता रहा, कंकड़ लगा एक चिड़िया के भी नहीं। नीम की छोटी-छोटी टहनियों से पत्तियाँ जरूर झड़-झड़कर गिर रही थीं।
उस बड़े आँगन के चारों तरफ छोटे-बड़े कमरे थे। केवल एक कोने पर टूटी हुई दीवार थी और पुराने चूने के छोटे-छोटे ढोंके उसके नीचे इधर-उधर पड़े थे। यह टूटी हुई दीवार दो-तीन हाथ ऊँची होगी। इसके नीचे होकर आँगन के पानी का बहाव था और बाहर लगा हुआ नाबदान। नाबदान एक बड़े से खंडहर में था। उस खंडहर में झाड़ी-झंखाड़ था, जहाँ होकर कम-से-कम गाँव के जानवर तो आँगन में नहीं आ सकते थे।
चिड़ियाँ चहचहाहट करती हुई टूटी दीवार के बाहरवाले झाड़ों पर कुदकने-फुदकने लगीं। दीपू ने उधर भी कंकड़ सन्नाए। चिड़ियाँ वहाँ से उड़कर आँगन के कमरों की खपरौल पर चीं-चीं कर उठीं। वहीं बगल में खपरैलवाला रसोईघर था। चिड़ियाँ उस पर पहुँचने से क्यों चूँकतीं ! दीपसिंह ने उस ओर भी कंकड़ फेंके। रसोईघर के छप्पर पर गिरे। उसकी माँ आँगन में निकल आई।
मंजरी की आयु छब्बीस-सत्ताईस के लगभग होगी। बड़ी-बड़ी आखोंवाली गोरी-साँवली; छरेरी सुंदर आकृति की थी। बहुत स्वस्थ थी। माथे पर कार्तिक स्नान की चंदन-खौर को आतंकमय बनाने का प्रयत्न करने पर भी मंजरी को डरावना न बना सकी। चिल्लाई, ‘टाट पर बस्ता खुला पड़ा है, चिड़ियों के पीछे पकड़कर आँगन भर में कंकड़ बिखेर रहा है ! पढ़ता क्यों नहीं रे ?’
‘कापी-किताबों पर चिड़ियों ने बीट कर दी तो ? फिर इतना हल्ला कर रही हैं कि पढ़ नहीं पाता हूँ।’ दीपू ने मुँह बिगाड़कर कहा।
‘कितने हरे-हरे पत्तें गिरा दिए तूने ! क्यों सत्यानास पर तुला है ?’
‘यह लो ! दातूनें तोड़ती हो तब तो ढेर सारे पत्ते गिर जाते हैं।’
‘आने दे उन्हें, तेरी मरम्मत कराऊँगी।’
‘लो, मैं पढ़ता तो हूँ। वैसे ही लगी हो। वह देखो, चिड़ियाँ रसोईघर के खपरों को गंदा कर रही हैं।’
दीपसिंह गुलेल एक तरफ रखकर बस्ते के पास बैठ गया और पढ़ने-लिखने की सामग्री इधर-उधर करने लगा। मंजरी रसोईघर में चली गई। दीपसिंह ने सोचा, गुलेल जहाँ की तहाँ टाँग दूँ। थोड़ा सा प्रयत्न करने पर सफल हो गया। कुछ ही क्षण पीछे चिड़ियाँ फिर चाँय-चाँय करती हुई नीम पर आने-जाने लगीं। उसने आसपास से कंकड़ उठा-उठाकर चिड़ियों को फेंकने शुरू किए; परंतु रसोईघर की दिशा में नहीं चलाए।
उसका पिता कहीं गाँव में गया था, जिसका भय मंजरी उस धमकी में छोड़ गई थी। सामने पौर थी। आहट मिली, जैसे कोई आ रहा हो। दीपू ने तुरंत एक पुस्तक खोलकर इस प्रकार हाथ में ली जैसे बड़ी लगन के साथ पढ़ रहा हो।
आनेवाले ने पौर से ही पुकारा, ‘मालिक हैं ?’
दीपसिंह ने पुस्तक अलग रख दी। बोला, ‘कौन है ?’
आगंतुक आँगन में आ गया।
‘क्या है, दमरू ?’ दीपसिंह ने पूछा।
दमरू अधेड़ अवस्था का दुबला सा व्यक्ति था। स्वास्थ्य उससे कभी का विदा ले चुका होगा। चेहरे पर शिकनें थीं। फटे साफे के नीचे से अधभूरे बाल झाँक रहे थे। ठोड़ी पर उसी रंग की दस-बीस दिन की हजामत होगी।
‘मालिक हैं, भैया सा’ब ?’ उसने प्रश्न दुहराया।
‘क्यों ?’
‘तिल्ली की झार-फूँक करवानी है। आज बुधवार है न।’
‘वह तो कहीं गाँव में देर के निकल गए हैं। बैठ जाओ, आते ही होंगे।’
दमरू आँगन की पौरवाली दीवार से सटकर बैठ गया। दीपू ने पढ़ना-लिखना शुरू ही नहीं किया था, बातें करने लगा, ‘कब से है तुम्हें तिल्ली ?’
‘न जाने कब से है, भैया। अब बढ़ गई है।’
‘कोई दवा खाई ?’
‘बहुत सी खा लीं, कुछ नहीं हुआ। अब तो दवा के लिए पैसा ही गाँठ में नहीं है।’
‘झारा-फूँकी से जरूर फायदा होगा। हमारे पिताजी बात-की-बात में छू कर देंगे।’
‘इसलिए तो आया हूँ, भैया सा‘ब’।
मंजरी चौके से फिर निकल आई। बोली, ‘पहले नीम की डालें तोड़ रहा था, अब बातें मठोल रहा है। पढ़ने-लिखने से तो तूने बैर कर रक्खा है।’
दीपू ने बात बनाई, ‘पढ़ तो रहा था, बिलकुल पढ़ रहा था। इतने में दादा को यह दमरू पूछते आ गए।’
दीपू ने एक पुस्तक खोल ली, जैसे पढ़ने के लिए तल्लीन होने वाला हो। धीरे-धीरे मरमराता रहा, ‘नीम की मैंने कौन सी डाल तोड़ी है ! उँह !’
मंजरी ने कुछ रुलाई के साथ दमरू से कहा, ‘गाँव में ढूँढ़ लो उन्हें। या बैठना हो तो पौर में जा बैठो, लड़के से बात न करो, पढ़ रहा है।’
दमरू खाँसता-साँस भरता चला गया। मंजरी रसोईघर में लौट गई। दीपसिंह ने पुस्तक बंद कर दी और एक कॉपी पर कुछ रेखाएँ खींचने-बनाने लगा।
दमरू पौर में नहीं बैठा, बाहर निकल गया। तिल्ली या किसी बीमारी से बढ़कर उसे चिंता अपने काम-मजूरी की थी। आज बुधवार को झाड़ा-फूँकी न करवा पाई तो अगले रविवार के दिन देखा जावेगा-सोचता जा रहा था कि पड़ोस में लुहार की दूकान से एक गूँज कान में पड़ी।
लुहार की दूकान उस घर से थोड़ी ही दूर पर थी। जरा चले, एक गली में मुड़े कि नत्थू लुहार की दूकान। दमरू दरवाजे से झाँककर आड़ में खड़ा हो गया। ‘राम-राम, मालिक’ कहकर अदब की आँखों दूकान के भीतर दृष्टि फेरने लगा। एक तरफ चढ़ी अवस्था का तगड़ा लुहार ऊँची-चौड़ी निहानी पर हथौड़े से खुरपी-हँसिए पीट रहा था। धौंकनी एक बुढ़िया चला रही थी। जब नत्थू भट्ठी में से औजार निकालता तभी बुढ़िया का हाथ रुकता था। दूसरी ओर काठ की छोटी सी तिपाई पर बैठा अंगद बीड़ी पी रहा था, जिसे दमरू ने ‘राम-राम, मालिक’ की थी; जिसके उत्तर में उसने केवल जरा सा सिर हिलाया था। अंगद की आँखें मदीली थीं, रसभरी-सी बड़ी-बड़ी। गोरे चेहरे पर चेचक के दागों में एकाध रेखा आ बैठी थी। आयु वैसे अधिक न होगी, वही कोई तीस-बत्तीस साल की। हथौड़े की चोटों और बीड़ी की फूँकों के बीच बातें चल रही थीं।
नत्थू ने कहा, ‘अखबारों में तो बड़ी गरम खबरें छपने लगी हैं। सुनते हैं कि....’
अंगद ने बात काटकर समाधान किया, ‘अरे मिस्त्री, अखबारी टप्पे हैं। देश के एक-तिहाई में तो रियासतें ही हैं, बाकी को जमींदार पाटे हुए हैं। भगवान् ने जमींदार और राजा मिटने के लिए नहीं बनाए हैं।’
नत्थू की थोड़ी सी भूमि थी और उसकी दूकान पर अधिकांश किसान ही आया करते थे। समाचार-पत्रों में छपी बातें घूमती-फिरती उसके यहाँ भी आ जाती थीं। किसान भी मिटने के लिए नहीं बनाए गए हैं, उसके मन में उठा। बोला, ‘मिटता कोई नहीं है।’
अंगद ने उसे बीड़ी दी, काम बंद हुआ। प्रसंग चलता रहा।
नत्थू कहता रहा, ‘हाँ-आँ, जो कुछ इतने जुगों से चला आ रहा है, फूँक मारने से तो मिटता नहीं। पर भगवान् की माया विचित्र है, पहाड़ का तिल और तिल का पहाड़ वे ही कर देते हैं। आदमी बिचारा क्या कर सकता है ?’
अगंद अपनी धुन में था-
‘रईसों के पुरखों ने रियासतें और हमारे पुरखों ने भूमि रक्त की नदियाँ बहाकर कमाई हैं। ऐसे ही नहीं मिट सकतीं।’ हलकी सी हँसी से उसने अपना तर्क चिकना कर लिया।
नत्थू बहस नहीं करना चाहता था, उसे अभ्यास ही न था। पर उसने इससे कुछ उलटा सुन रखा था, कुछ देखा भी था। कहा, ‘भगवान् जो चाहते हैं वही होता है।’ और वह फिर हथौड़ा चलाने लगा।
अंगद मझोले दरजे का जमींदार था। पचास एकड़ के लगभग होगी उसकी भूमि। समझता अपने को जरा बड़ा था, ऊँची जाति का था ही। दमरू ने वहीं से हाथ जोड़कर उसे अपनी ओर आकृष्ट किया।
‘क्या है, दमरू ?’ अंगद ने बिना किसी रुचि के पूछा।
दमरू ने गिड़गिड़ाकर कहा, ‘आज बुधवार है, मालिक, झड़वाने् आया हूँ।’
अंगद की उन मदीली आँखों में दर्प और दंभ दोनों आ गए, ‘सो यह समय है झाड़ा-फूँकी का ! बड़े भोर आना चाहिए था।’
नत्थू हाथ रोककर बोला, ‘न जाने कितने गरीब निहाल हो गए हैं आपके हाथ से। कर दीजिए बिचारे का भला।’
उस गरीब से अधिक उस क्षण नत्थू अपना भला करना चाहता था, जमींदार जी चले जाएँ तो अपना काम बेखटके करता रहूँ।
‘हाँ, मालिक, बड़ा जस है आपके हाथ में।’ दमरू ने निवेदन किया।
अंगद साँप काटे की, तिल्ली की और न जाने कितने मर्जों की झाड़ा-फूँकी किया करता था। इधर-उधर की जड़ी-बूटियाँ भी कभी-कभी प्रयोग में लाता था। कुछ अच्छे हो गए, कुछ मर गए। जो अच्छे हो गए थे वे उसके करतब से, जो मर गए वे अपने भाग्य से।
बीड़ी का अंतिम टुकड़ा, जिसमें तंबाकू का एकाध कण मात्र रह गया होगा, फेंककर अंगद मूँछों पर हाथ फेरता हुआ कुछ सोचने लगा।
‘अच्छा, चलो घर।’ अंगद ने दमरू से कहा और दूकान से बाहर निकल आया। दमरू उसके पीछे हो लिया।
पौर में पहुँचकर दमरू से अप्रत्याशित कोमल स्वर में बोला, ‘यहीं बैठ जाओ, मैं हाथ-पाँव धोकर आता हूँ।’
दमरू बैठ गया। कितने अच्छे हैं मालिक, उसने सोचा।
अंगद ने आँगन में जाकर हाथ-पाँव धोए।
आहट पाकर मंजरी रसोईघर से निकल आई। मुसकराकर बोली, ‘कलेवा कर लो।’
दीपसिंह, जो अभी कॉपी पर रेखाएँ खींच रहा था, बोला, ‘दमरू तिल्ली का रोग झड़वाने आया है, वह कब तक बैठा रहेगा ?’
‘ओ हो ! सारे जग की चिंता है न तुझे !’ मंजरी के स्वर में मिठास थी।
‘तुमने कलेवा कर लिया, बेटा ?’ अंगद ने पूछा।
‘नहीं तो, भोर से लिखने-पढ़ने में जो लगा हूँ।’ दीपू ने उत्तर दिया।
‘हाँ-हाँ, बड़ा पढ़नेवाला है ! तभी से गुलेल चला रहा है यह !’ मंजरी के होंठों पर मुसकान थी।
कॉपी पर आँख घुमाते हुए अंगद ने दीपू को शाबाशी दी, ‘कॉपी पर आर्ट बना रहा है, जिसे लोग कला कहते हैं। किसी दिन बड़ा कलाकार होगा दीप।’
‘अहा हा-हा ! जरूर होगा। ऐसे ही बिगाड़े जाओ इसे।’ मंजरी की भर्त्सना में खीज जरा भी न थी। उसने अंगद से कलेवा करने का फिर अनुरोध किया।
‘दमरुआ का मंत्र-जंत्र करके अभी आता हूँ। तब तक तुम कलेवा कर लो, बेटा। स्कूल का समय भी होने को है। हाथ-पाँव धो लिये हैं; पहले यह काम कर लूँ।’ कहकर अंगद पौर में चला गया।
दीपू का चाहे मन लग रहा हो, चाहे दिखलावे के लिए हो, वह कॉपी पर कला की रेखाएँ बनाता रहा।
अंगद ने झाड़ा-फूँकी के बाद दमरू को कुछ परहेज बतलाकर बातचीत की, ‘आज काम पर कहाँ जाना है ?’
दमरू के पास निज का कोई खेत न था। जिसके यहाँ मजूरी पर जाना था। उसका नाम बतला दिया।
‘हमारे यहाँ करोगे काम सोंझ-बटाई पर ?’ जैसे ही अंगद से पूछा, दमरू ने धरती पर सिर टेककर हामी भरी और हाथ जोड़कर बैठ गया।
अंगद ने सोंझ की शर्ते बतलाईं, ‘एक हिस्सा तुम्हारा और तीन हमारे। हमारी भूमि बहुत बढ़िया है। बैल-बीज वगैरह भी हमारे रहेंगे, तुम्हें तो खेत बनाने भर हैं। आजकर उसमें पानी भरा है। धीरे-धीरे सूख रहा है। बखरकर बीज बोना भर है। थोड़ी सी निदाई, रखवाली वगैरह। सो तुम सब जानते ही हो।’
दोनों तरह की ‘वगैरह’ में जो कुछ लुका-छिपा था उसे दमरू जानता था, तो भी अंगद ने थोड़ा सा ब्योरा दिया।
दमरू अब भी हाथ जोड़े बैठा था।
‘जमीन का लगान, मालगुजारी और बीज की सवाई काटकर गल्ला और भूसा बाँट लिया जाएगा। कटाई तुम्हारे जिम्मे रहेगी, खलिहान का काम-धाम तो खैर करोगे ही।’
दमरू के जुड़े हुए हाथ कुछ ढीले पड़ गए। फिर भी उसने हामी भरी और नम्रता के साथ अपनी एक कठिनाई पेश की, ‘मालिक, फसल आने तक हमारे खाने के लिए ?’
दमरू के स्वर में अंगद को कुछ निर्बलता भासित हुई।
‘हम देंगे। वाह ! भूखों थोड़ी मरने देंगे। जैसे ही फसल कटने पर अनाज गाहा, तुम्हारे हिस्से में से इन दिनों की खवाई सवाई समेत काट लेंगे। कायदा है न !’
‘सवाई समेत, मालिक ?’
‘अच्छा भई, सवाई नहीं, रुपए के अठारह आना, बस ?’
दमरू ने हामी भरी।
भीतर से कलेवा करने का तकाजा फिर हुआ।
‘मैं तुम्हारी तिल्ली को ठीक करके रहूँगा। बैठना, तुम्हारे लिए भी कलेवा आता है।’ आश्वासन देकर अंगद भीतर चला गया।
पराँठे बने थे। अंगद कलेवा करने लगा। चेहरे पर प्रसन्नता की लहर थी।
मंजरी ने कहा, ‘कार्तिक की पूनो आ रही है।’
‘हाँ-हाँ, हर साल कार्तिक नहाती हो और पूनो आती है।’
‘इस साल जरा अच्छी सी साड़ी आनी चाहिए।’
‘जरूर आएगी,’ अंगद ने मुसकराते हुए भरोसा दिया।
मंजरी ने दीपू को बुलाया और उसके हाथ में दमरू के लिए बासी रोटियाँ दे दीं। दीपू ने अपने लिए भी कलेवा लिया और साथ में आम का अचार। पौर में जाकर उसने रोटियों के साथ दमरू को अपने कलेवे में से एक पराँठा और आम का अचार दे दिया। फिर आंगन में जाकर बचे हुए पराँठे चल-फिरकर धीरे-धीरे खाने लगा। बस्ता बिखरा पड़ा था। चिड़ियाँ चहक-चहककर उड़ रही थीं। उसे स्कूल पहुँचने की जल्दी न थी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i