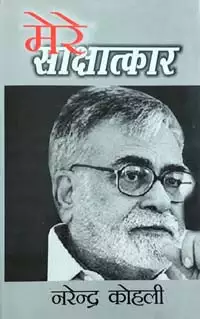|
लेख-निबंध >> जहाँ है धर्म वहीं है जय जहाँ है धर्म वहीं है जयनरेन्द्र कोहली
|
12 पाठक हैं |
|||||||
महाभारत के कथानक को, उसकी ‘अर्थ-प्रकृति’ को समझने का प्रयत्न
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रस्तुत पुस्तक को महाभारत के कथानक को,
उसकी अर्थप्रकृति
को समझने का प्रयत्न कहा जा सकता है तथा एक उपन्यासकार के कथानक-निर्माण
के सारे उपकरणों तथा तर्क-युक्तियों को परखने का कर्म भी। पुस्तक रूप में
लम्बे आख्यान को माध्यम से लेखक ने व्यास के मन में झाँकने का प्रयास किया
है। लेखक के अनुसार जब उसने महाभारत को साहित्यिक कृति के रूप में पढ़ना
प्रारंभ किया था तो उनके मन अनेक प्रश्न थे। लेकिन पढ़ते-पढ़ते जब महाभारत
उस पर आच्छादित होने लगा तो उसने महसूस किया कि यदि स्वयं को महाभारत पर आरोपित करने का प्रयत्न करता है तो महाभारत मौन है, और यदि जिज्ञासु बनकर उसके सम्मुख जाता है तो वह उनकी समस्याओं का समाधान करता है।
लेखकीय
किसी ग्रंथ का अध्ययन वस्तुतः क्रिया और प्रतिक्रिया की दोहरी और जटिल
प्रक्रिया है। विशेषकर जब ग्रंथ काल की कसौटी पर अपना महत्त्व सिद्ध कर
चुका हो। इस प्रक्रिया में एक सीमा तक ग्रंथ हम पर आरोपित होता है; और
दूसरी ओर हम अपने-आप ग्रंथ को आरोपित करते हैं। यही कारण है कि किसी एक
ग्रंथ को सारे पाठक एक ही रूप में नहीं पढ़ते।
महाभारत को उसके मूल रूप में पढ़ने से पहले भी उससे मेरा परिचय था। हम सब का ही होता है।...कुछ श्रुति-पंरपरा से, कुछ महाभारत-कथा पर आधृत साहित्यिक कृतियों के माध्यम से, और कुछ सामाजिक मान्यताओं के माध्यम से ! यही कारण है कि मैंने पाया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपनी-अपनी राम-कथा के समान अपनी-अपनी पांडव-कथा भी है, जो व्यास की कथा से भिन्न भी हो सकती है, कुछ पात्र प्रिय होते हैं, कुछ उक्तियां भाती हैं और कुछ धारणाएं मुग्ध करती हैं...किंतु शिकायतें भी तो कम नहीं होतीं। जब हम अपनी बुद्धि, ज्ञान और चिंतन को उस समय-सिद्ध चरित्रों और घटनाओं पर आरोपित करते हैं, तो हम स्वयं अपने मन में उन से कुछ बड़े तो हो जाते हैं, किंतु न तो तटस्थ भाव से उन चरित्रों और घटनाओं को, उनके अपने रूप में जानने का प्रयास करते हैं, और न ही उन ग्रंथों को अपना संभावित विकास कर पाते हैं। वह तो तभी संभव हो सकेगा, जब उन पात्रों को उन्हीं के देश-काल और मनोविज्ञान में रख कर, उनसे परिचय प्राप्त किया जाए।
मैंने महाभारत को श्रेष्ठ साहित्य की एक कृति के रूप में ही पढ़ना आरंभ किया था।... और उस समय मेरे मन में प्रश्न भी अनेक थे। पढ़ते-पढ़ते जब महाभारत मुझे आच्छादित करता चला गया, तो मेरी समझ में यह भी आया कि मैं स्वयं को महाभारत पर आरोपित करने का प्रयत्न करता हूं, तो महाभारत मौन है; किंतु यदि मैं जिज्ञासु बनकर उसके सम्मुख जाता हूं, तो वह मेरी समस्याओं का समाधान करता है।...मैंने यह भी पाया कि मेरे प्रश्न, मेरी आपत्तियां, मेरी जिज्ञासाएं-सब एक कथाकार के रूप में ही हैं; और मेरा सारा प्रयत्न उस कथानक को उसके मूल रूप में समझने का ही है।
और जो कुछ मैं समझ पाया, वह इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है। यह पुस्तक उपन्यास के रूप में नहीं है; किंतु उपन्यास की सामग्री का परिचय देने का एक भरपूर प्रयत्न अवश्य है। इसे महाभारत के कथानक को, उसकी ‘अर्थ-प्रकृति’ को समझने का प्रयत्न भी कहा जा सकता है; और एक उपन्यासकार के कथानक-निर्माण के सारे उपकरणों तथा तर्क-युक्तियों को परखने का कर्म भी। विद्वान होने का दावा मुझे कभी नहीं रहा। मैंने इस लंबे आख्यान के माध्यम से व्यास के मन में झांकने का प्रयत्न किया है...संभव है, इसमें से कहीं-कहीं मेरा अपना मन भी झलकता हो।
महाभारत को उसके मूल रूप में पढ़ने से पहले भी उससे मेरा परिचय था। हम सब का ही होता है।...कुछ श्रुति-पंरपरा से, कुछ महाभारत-कथा पर आधृत साहित्यिक कृतियों के माध्यम से, और कुछ सामाजिक मान्यताओं के माध्यम से ! यही कारण है कि मैंने पाया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपनी-अपनी राम-कथा के समान अपनी-अपनी पांडव-कथा भी है, जो व्यास की कथा से भिन्न भी हो सकती है, कुछ पात्र प्रिय होते हैं, कुछ उक्तियां भाती हैं और कुछ धारणाएं मुग्ध करती हैं...किंतु शिकायतें भी तो कम नहीं होतीं। जब हम अपनी बुद्धि, ज्ञान और चिंतन को उस समय-सिद्ध चरित्रों और घटनाओं पर आरोपित करते हैं, तो हम स्वयं अपने मन में उन से कुछ बड़े तो हो जाते हैं, किंतु न तो तटस्थ भाव से उन चरित्रों और घटनाओं को, उनके अपने रूप में जानने का प्रयास करते हैं, और न ही उन ग्रंथों को अपना संभावित विकास कर पाते हैं। वह तो तभी संभव हो सकेगा, जब उन पात्रों को उन्हीं के देश-काल और मनोविज्ञान में रख कर, उनसे परिचय प्राप्त किया जाए।
मैंने महाभारत को श्रेष्ठ साहित्य की एक कृति के रूप में ही पढ़ना आरंभ किया था।... और उस समय मेरे मन में प्रश्न भी अनेक थे। पढ़ते-पढ़ते जब महाभारत मुझे आच्छादित करता चला गया, तो मेरी समझ में यह भी आया कि मैं स्वयं को महाभारत पर आरोपित करने का प्रयत्न करता हूं, तो महाभारत मौन है; किंतु यदि मैं जिज्ञासु बनकर उसके सम्मुख जाता हूं, तो वह मेरी समस्याओं का समाधान करता है।...मैंने यह भी पाया कि मेरे प्रश्न, मेरी आपत्तियां, मेरी जिज्ञासाएं-सब एक कथाकार के रूप में ही हैं; और मेरा सारा प्रयत्न उस कथानक को उसके मूल रूप में समझने का ही है।
और जो कुछ मैं समझ पाया, वह इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है। यह पुस्तक उपन्यास के रूप में नहीं है; किंतु उपन्यास की सामग्री का परिचय देने का एक भरपूर प्रयत्न अवश्य है। इसे महाभारत के कथानक को, उसकी ‘अर्थ-प्रकृति’ को समझने का प्रयत्न भी कहा जा सकता है; और एक उपन्यासकार के कथानक-निर्माण के सारे उपकरणों तथा तर्क-युक्तियों को परखने का कर्म भी। विद्वान होने का दावा मुझे कभी नहीं रहा। मैंने इस लंबे आख्यान के माध्यम से व्यास के मन में झांकने का प्रयत्न किया है...संभव है, इसमें से कहीं-कहीं मेरा अपना मन भी झलकता हो।
प्रथम खंड
‘महाभारत’ के आरंभ को, घटना तथा आख्यान-शिल्प-दोनों
दृष्टियों से देखा जा सकता है। स्वयं ‘महाभारत’ में
ही आख्यान-शिल्प की दृष्टि से इस रचना का आरंभ तीन बार वर्णित हैः प्रथम,
वेदव्यास द्वारा इसकी रचना, तथा गणनायक गणेश द्वारा इसका लेखन; द्वितीय,
जनमेजय के नागयज्ञ में, जनमेजय की इच्छानुसार व्यास-शिष्य वैशम्पायन
द्वारा व्यास-रचित कृति का वाचन; तथा तृतीय, नैमिषारण्य में कुलपति शौनक
के यज्ञ में लोमहर्षण-पुत्र उग्रश्रवा सौति द्वारा इसका आख्यान। वस्तुतः
ये तीन आरंभ-बिंदु, ‘महाभारत’ को तीन भिन्न रूप
प्रदान करते हैं; और ये तीन आरंभ-बिंदु इस तथ्य के प्रकाश में और भी
महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं कि विद्वान् व्यास-लिखित मूल ग्रंथ
‘जय’ में दो बार संवर्द्धन स्वीकार करते हैं।
वेदव्यास रचित कृति का नाम ‘जय’ था; और उसे काव्य कहा गया है। उसका सृजन काव्य के ही रूप में हुआ, ‘‘हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान इत्यादि से शरीर-शुद्धि करके पवित्र हो, कुश का आसन बिछा कर बैठे थे। उस समय नियम-पालनपूर्वक शांत-चित्त हो, वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थिति हो, उन्होंने धर्मपूर्वक महाभारत-इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान-दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा।’’(28 तथा 29 के मध्य के श्लोक/1, आदि-पर्व)
हम अनेक बार घटित घटनाओं का एकान्त में स्मरण करते है; अथवा पुरानी घटनाओं की चर्चा करते हैं। किंतु व्यास की यह स्थिति भिन्न है। यह स्मरण अथवा पुनरावलोकन मात्र नहीं है। इसमें व्यास ध्यान-योग में स्थित हैं और ज्ञान-दृष्टि द्वारा धर्मपूर्वक महाभारत-इतिहास के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। यह वस्तुतः रचना का गर्भाधान है। अभी रचना को अभिव्यक्त नहीं किया गया है, न उसे शब्दबद्ध किया गया है, न लिपिबद्ध-किंतु, व्यास ने उसे मन में रच लिया है। वे ब्रह्मा से कहते हैं, ‘‘मैंने संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाभारत की रचना की है। ब्रह्मन ! मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्तवत रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उसके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उसका प्रशस्त रूप प्रकट किया है।’’ (61-63/1, आदिपर्व) और फिर ब्रह्मा के ही परामर्श के अनुसार उन्होंने गणेश से कहा, ‘‘गणनायक ! आप मेरे द्वारा निर्मित इस ‘महाभारत’ ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा। मैंने मन-ही-मन इसकी रचना कर ली है।’’(77/ 1, आदिपर्व)
‘महाभारत’ संबंधी आज की मान्यताओं के अनुसार व्यास द्वारा रचित उस प्रथम रचना का नाम ‘जय’ था; किंतु इस श्लोकों में उसे ‘महाभारत’ ग्रंथ कहा गया है। बहुत संभव है कि यह श्लोक भी बाद के किसी संवर्द्घन का ही अंग हो; क्योंकि ग्रंथ का नाम ‘जय’ से ‘महाभारत’ तो हो सकता है, ‘महाभारत’ से ‘जय’ नहीं हो सकता। फिर भी इतना स्पष्ट है कि वह कृति ‘काव्य’ है। ब्रह्मा कहते हैं, ‘‘तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब यह काव्य नाम से ही प्रसिद्ध होगी।’’ (72/1, आदिपर्व) किंतु यह काव्य, इतिहास पर आधृत है और इसमें वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों का तत्त्व भी सम्मिलित किया गया है। अतः यह इतिहास का आलेख मात्र नहीं है, यह घटनाओं का वर्णन मात्र नहीं है-यह एक काव्य है, जिसकी वेदव्यास ने रचना की है। रचना वे रच चुके हैं, अतः किसी की इच्छा, प्रसन्नता अथवा आवश्यकता के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। यह उन्होंने किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को ध्यान में रख कर किसी अवसर अथवा आवश्यकता विशेष के लिए नहीं रची है। वे किसी से संबोधित नहीं हैं। उन्होंने इसकी रचना स्वांतःसुखाय ही की है। उनके सम्मुख कोई श्रोता नहीं है, केवल उनके लिपिकार अथवा लेखक, गणपति गणेश बैठे हैं। इसलिए इस रचना का कोई तात्कालिक लक्ष्य अथवा उद्देश्य नहीं है। किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को किसी एक विशिष्ट स्थिति से उबारने, किसी समस्या का समाधन करने, अथवा किसी विशिष्ट जीवन-दृष्टि की स्थापना का प्रयास किया गया है।
इस कृति का नाम है ‘जय’। असत्य पर सत्य की जय, अधर्म पर धर्म की जय। क्योंकि इसके विपरीत की स्थापना करने की आवश्यकता किसी और को हो तो हो, कवि को नहीं है। कवि के रूप में व्यास ने भी यही किया। अतः इस दृष्टि से इस मूल रचना ‘जय’ में घटनाओं की दृष्टि से कौरवों तथा पांडवों के युद्ध का वर्णन किया गया होगा, जिसमें पांडवों की विजय का उल्लासपूर्ण चित्रण होगा। इसमें पांडवों की वीरता और उसके गुणों को प्रस्तुत किया गया होगा, ताकि पाठकों के संस्कारों का परिष्कार हो। यह एक कवि की रचना होगी, जिसमें काव्य के गुणों का समावेश नहीं होगा। अतः इसमें घटना की दृष्टि से युद्ध के पश्चात विजयी होकर पांडवों द्वारा प्रजा के पालन और जीवन के सुखों के भोग का चित्रण होगा। क्षत्रिय कार्यों की प्रशंसा होगी। युद्ध-कर्म पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया गया होगा। उसके विषय में संशय नहीं प्रकट किया गया होगा। स्वयं वासुदेव कृष्ण जिस युद्ध की प्रेरणा थे, जिसे वे धर्म-युद्ध मानते थे, जिस युद्ध पांडवों की विजय के लिए वे अर्जुन के सारथि बने थे-उस युद्ध को व्यास ने निरर्थक नहीं माना होगा। यद्यपि ‘महाभारत’ को बाद में आरण्यक संस्कृति का ग्रंथ कहा गया, किंतु ‘जय’ शीर्षक धारण करने वाला काव्य आरण्यक-संस्कृति वाहक नहीं रहा होगा।
महाभारत जैसे युद्ध-काव्य में रूरू और डुडुंभ के वार्तालाप के माध्यम से ‘अहिंसा’ की महत्ता का प्रवेश कराया गया है और रूरू की जिज्ञासा के फलस्वरूप उसे जनमेजय की कथा सुनाई गई है। यह कदाचित् ‘भारत’ इतिहास का आरंभ है। किंतु ‘भारत’ इतिहास की रचना किसी एकान्त स्थान पर बैठकर किसी कवि की अंतर्प्रेरणा तथा आत्म-संतोष के लिए नहीं हुई है। अब ‘जय’ नामक काव्य एक विशिष्ट संदर्भ से जुड़ गया है। काव्य के स्थान पर इतिहास प्रमुख हो गया है। आर्यों और नागों में शत्रुता की चरम स्थिति पहुँच चुकी है। हस्तिनापुर के आर्य सम्राट जनमेजय ने अपनी प्रतिहिंसा में नागों को समूल नष्ट करने का संकल्प किया है। वह एक बड़े जातीय युद्ध के द्वार पर खड़ा है। ऐसे में अपने पूर्वजों का गौरवज्ञान सुनना चाहता है। युद्ध से पहले उनकी वीरता को अनुभव करना चाहता है।
उन घटनाओं के प्रत्यक्ष द्रष्टा तथा काव्य के रूप में उनके स्रष्टा वेदव्यास स्वयं वहाँ विद्यमान हैं। जनमेजय उनसे वह काव्य सुनना चाहता है। उपर्युक्त अवसर पर उसे सुनने का उद्देश्य मात्र रसास्वादन नहीं है। बागों के विरूद्ध इस युद्ध का औचित्य सिद्ध करने तथा अपने लिए युद्धोन्माद का बल पाने के लिए वह ‘जय’ काव्य सुनना चाहता है।
किंतु वेदव्यास के लिए जनमेजय और नागों का युद्ध, धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं था। वह जातीय युद्ध था, जिसमें एक जाति प्रतिशोध के लिए प्रति-हिंसावश अपने शस्त्र बल से दूसरी जाति को मिटा देना चाहती थी। निश्चित रूप से वेदव्यास, एक ओर आर्य सम्राट जनमेजय का उत्साह खंडित नहीं करना चाहते होंगे और दूसरी ओर वे युद्धोन्माद की अग्नि को प्रचंड करना भी श्रेय़स्कर नहीं मानते होंगे। उन्होंने कौरवों और पांडवों के युद्ध में धर्म की विजय का उद्घोष किया था। यदि संभव होता तो स्वयं वासुदेव कृष्ण और कृष्ण द्धैपायन व्यास युद्ध के स्थान पर धर्माधत संधि ही चाहते। दुर्योधन ने उसे संभव नहीं होने दिया; आर्यों तथा नागों में प्रश्न धर्म और अधर्म पक्ष का नहीं था। यहाँ भेद जाति का था और व्यक्ति की प्रतिहिंसा जाति का द्वेष बन गई थी। दोनों जातियाँ प्रतिशोध का भाव त्याग कर क्षमा और उदारता के आधार पर संधि कर सकती थीं। इस समय वेदव्यास ने आर्यों और नागों में किसी सम्मानजनक संधि की ही कामना की होगी।
उन्होंने अपने शिष्य से कहा, ‘‘वैशम्पायन ! पूर्वकाल में कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, जिसे तुम मुझ से सुन चुके हो, यह सब इन राजा जनमेजय को सुनाओ।’’ (22/60, आदिपर्व)
महाभारत के वर्णन के अनुसार, ‘‘उस समय गुरूदेव व्यास जी की आशा पाकर विप्रवर वैशम्पायन ने राजा जनमेजय, सभासदगण तथा अन्य सब भ्रूपालों से कौरव-पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी और उसका सर्वनाश हुआ-वह सब पुरातन इतिहास कहना आरंभ किया।’’(23-24/60, आदिपर्व)
अब यह इतिहास है-‘भारत’ इतिहास ! इसे काव्य नहीं कहा गया। इस इतिहास के मूल में फूट की चर्चा है, फूट के कारण युद्ध और युद्ध के कारण सर्वनाश का उल्लेख है। निश्चित रूप से सर्वनाश करने वाले ‘युद्ध’ का समर्थन न वेदव्यास करेंगे, न उनके शिष्य वैशम्पायन; किंतु एक क्षत्रिय राजा के सम्मुख वे युद्ध का निषेध भी नहीं कर सकते। अतः युद्ध के परिणामों के प्रति सावधान करने के लिए युद्धोन्मुख राजा ही सर्वोत्तम पात्र है। वैशम्पायन कहते हैं, ‘‘जनमेजय ! तुम इस महाभारत कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो और मुझे यह कथा उपलब्ध है, तथा श्रीगुरूजी के मुखारविन्द से मुझे यह आदेश भी मिल गया है कि मैं तुम्हें यह कथा सुनाऊं। इससे मेरे मन को बड़ा उत्साह प्राप्त होता है। राजन् ! जिस प्रकार कौरवों और पांडवों में फूट पड़ी-वह प्रसंग सुनो। राज्य के लिए जो जुआ खेला गया, उससे उनमें फूट हुई और उसी के कारण पांडवों का वनवास हुआ। भरतश्रेष्ठ ! फिर जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत युद्ध हु्आ, वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुमसे कहता हूँ, सुनो।’’(3-5/61 आदिपर्व)
इस उक्ति में वैशम्पायन बहुत सावधान हैं। वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि युद्ध का मूल कारण राज्य है, उस राज्य के कारण फूट पड़ी और युद्ध हुआ; किंतु युद्ध से समस्या का समाधान हुआ या नहीं, सर्वनाश अवश्य हुआ। वैशम्पायन द्वारा सुनाए जा रहे ‘भारत’ में युद्ध को क्षत्रिय के काम्य लक्ष्य के स्थान पर विनाशकारी कर्म के रूप में रेखांकित किया जा रहा है। यहीं से महाभारत में ‘युद्ध’ को किसी समस्या के समाधान के रूप में देखने के प्रति संशय का भाव उत्पन्न हुआ होगा। यदि युद्ध को समस्याओं के समाधान के रूप में स्वीकार किया जाता तो आर्यों और नागों में भंयकर युद्ध होता, जिसमें संभवतः आर्यों की भी बहुत भारी क्षति होती; किंतु नागों का तो सर्वनाश होकर ही रहता। इसलिए सारे चिन्तकों तथा मनीषियों के द्वारा ‘युद्ध’ के स्थान पर राजनीतिक समाधान को ही वरीयता दी गई। जनमेजय ने आस्तीक को वरदान दिया। तक्षक को क्षमा किया गया; और नागों को सुखपूर्वक रहने की अनुमति दी गई।
दृष्टिकोण के इस परिवर्तन का प्रभाव कथा की रूपरेखा पर भी पड़ा होगा। वैशम्पायन की कथा में युधिष्ठिर को युद्ध के लिए और भी अनिच्छुक दिखाया गया होगा। युधिष्ठिर में आनृशंसता के भाव की वृद्धि की गई होगी और सबसे बड़ी बात है विजय के पश्चात भी निराशा, दुख तथा विषाद का हाथ लगना दिखाया गया होगा, जिससे युद्ध के प्रति उत्साह न बढ़े और युद्ध को विजय, उल्लास तथा सुख-भोग का सरल मार्ग न माना जाए। संभव है कि युद्धोपरांत निराशा तथा हताशा के सारे प्रसंग इसी अवसर पर या तो रचकर जोड़े गए हों; अथवा उन्हें रेखांकित कर विषाद का रंग गाढ़ा किया गया हो।
यहां एक आपत्ति यह की जा सकती है कि महाभारत के वर्णन के अनुसार, जनमेजय द्वारा यज्ञ रोक दिए जाने तथा तक्षक को क्षमा कर दिए जाने के पश्चात वेदव्यास का पदार्पण होता है। ऐसी स्थिति में यह कैसे माना जा सकता है कि यह प्रभाव वैशम्पायन द्वारा सुनाई गई कथा का था ?
पहली बात तो यही है कि तर्क-संगत निष्कर्ष निकालने के लिए पुराण कथाओं की शिथिलता को भी ध्यान में रखना चहिए। दूसरी बात यह है कि ‘महाभारत’ में भी यह स्पष्ट है कि वेदव्यास नाग-यज्ञ में ही पधारे थे। ‘महाभारत’ कथा सुनने के अंत तक आस्तीक भी वहीं था और कथा की समाप्ति के पश्चात ही यज्ञ को पूर्णतः समाप्त घोषित किया गया था और जनमेजय तक्षशिला से हस्तिनापुर लौटा था। न तो वेदव्यास टहलते हुए तक्षशिला पहुँचे थे और न ही वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि जनमेजय नाग-यज्ञ कर रहा है। यदि आस्तीक ने अपने उद्यम द्वारा यज्ञ को समाप्त करवा दिया होता तो जनमेजय महाभारत की कथा सुनने के लिए वहां बैठा नहीं रहता। वस्तुतः महाभारत की कथा जनमेजय को यज्ञ के मध्य ही सुनाई गई, जिससे उसकी समझ में आया होगा कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं होता।
वैशम्पायन द्वारा सुनाए गए इस ‘भारत’ इतिहास में निश्चय ही हिंसा तथा प्रतिहिंसा के अवमूल्यन का प्रयत्न किया गया होगा और अहिंसा की महिमा को स्थापित किया गया होगा।
महाभारत का तृतीय आरंभ जिस परिवेश में हुआ है, उसका वर्णन स्वयं महाभारत में इस प्रकार हैः ‘‘एक समय की बात है। नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के बारह वर्षों से चलते रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुख-पूर्वक बैठे थे,. सूत-कुल को आनन्दित करने वाले लोमहर्षण-पुत्र उग्रश्रवा सौति स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथा-वाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवा जी को उनसे चित्र-विचित्र कथाएँ सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया।’’(1-3/1, आदिपर्व)
इस वक्तव्य में अनेक बातें ध्यातव्य हैं। प्रथम तो यह कि नैमिषारण्य में कुलपति शौनक का आश्रम है, यहाँ सांसारिक चर्चाएं नहीं होतीं। दूसरे जो श्रोता वहां एकत्रित हैं वे ब्रह्मर्षि हैं। उनके जीवन का लक्ष्य ब्रह्म-प्राप्ति है। फिर वे लोग इस समय कुलपति शौनक के बारह वर्षों तक चलने वाले सत्र में पधारे हैं। निश्चित रूप से इस समय उनके मन और भी अधिक एकाग्र हैं तथा अपने लक्ष्य के प्रति और भी अनुकूलित हैं। इस समय वे कोई साधारण काव्य नहीं सुनना चाहते होंगे, न उनकी इच्छा युद्ध तथा शांति की समस्याओं पर वक्तव्य सुनने की होगी। वे अवकाश के क्षणों में हैं, अतः संभव है, वे कुछ बौधिक मनोरंजन भी चाहती हों।
सौति उग्रश्रवा उन्हीं से पूछते हैं कि वे क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि श्रव्य-काव्य तथा कथावाचन की परंपरा में वाचन में भी अधिक महत्त्वपूर्ण श्रोता का व्यक्तित्व, उसकी मनःस्थिति तथा उसकी तत्कालीन आवश्यकता है। उग्रश्रवा पूछते हैं, ‘‘इस समय आप सभी स्नान, संध्या-वंदन, जप तथा अग्निहोत्र आदि करके, शुद्ध हो, अपने-अपने आसन पर स्वस्थचित से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं ? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न-भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं स्मृतियों का पवित्र इतिहास।’’ (15-16/1, आदिपर्व)
ऋषियों ने अपनी रूचि प्रकट करते हुए कहा, ‘‘उग्रश्रवा जी ! परमर्षि द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास-रूप पुराण का वर्णन किया है, और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने-अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक-एक पद, वाक्य एवं, पर्व, विचित्र शब्द-विन्यास और रमणीय अर्थ से पूर्ण है, जिसमें आत्मा-परमात्मा के सूक्ष्म-स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी, ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली, पदों-वाक्यों की व्युत्पत्ति से मुक्त, सब शस्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनके समर्थित जो अद्भुतकर्म व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्यस्वरूपा है। पाप और भय का नाश करने वाली है ।’’(17-21/ 1, आदिपर्व)
स्पष्टताः इसमें इस कृति को ‘इतिहास’ कहा गया है। वस्तुतः ‘जय’ काव्य के पश्चात यह कृति ‘भारत’ नामक इतिहास हो गई-इसमें कोई संशय नहीं है; किंतु यह इतिहास, साधारण इतिहास नहीं है। इसमें अन्य अनेक गुणों के साथ-साथ ‘आत्मा-परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियाँ भरी हुई हैं। उग्रश्रवा के श्रोताओं की सबसे अधिक रूचि ‘आत्मा-परमात्मा के स्वरूप’ और उनके अनुभव की युक्तियों में ही हो सकती है। ‘‘उग्रश्रवा एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम तथा यथार्थ कथा कहने लगे।’’ (8/1, आदिपर्व) मुझे लगता है कि इस तीसरे वाचन ने इस कृति को ‘भारत’ से ‘महाभारत’ बना दिया। इसमें या तो इतिहास रह गया था अध्यात्म। उग्रश्रवा ने कहा, ‘‘शौनक जी ! आपके इस सतसंग सत्र में यह जो उत्तम इतिहास ‘महाभारत’ सुना रहा हूँ, यही जनमेजय के सत्र-यज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशम्पायन जी के द्वारा भी वर्णित किया गया था। (33/1, आदिपर्व) बहुत संभव है कि कुशल वक्ता और कथावाचक उग्रश्रवा ने इसमें अपनी दृष्टि के अनुकूल अनेक ऐतिहासिक-पौराणिक कथाएं जोड़ी हों। उन्होंने कहा, ‘‘जैसे भोजन किए बिना शरीर-निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इतिहास का आश्रय लिए बिना, पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है।’’(33/ 1, आदिपर्व) किंतु यह इतिहास उग्रश्रवा के लिए साध्य नहीं था, वह मात्र साधन ही था। संभवताः संवर्धन के इसी चरण में महाभारत की कथा मर्त्यलोक से स्वर्ग-लोक तक पहुँच गई। युधिष्ठिर आनृशंसता से भी आगे बढ़कर सम-दृष्टि को प्राप्त हो चुका था, जो अपने भाइयों को स्वर्गारोहण के समय गिरते हुए देखकर भी विचलित नहीं होता तथा अपने साथ आए हुए कुत्ते का त्याग कर स्वर्ग भी प्राप्त नहीं करना चाहता। यह उद्देश्य कदाचित आध्यात्मिक चिंतन से उद्भूत है, वह भौतिक भोगों की निरर्थकता तथा अधिकार के लिए लड़े गए युद्धों के लिए ही हिंसा की निस्सारता चित्रित कर, मनुष्य को अपनी सीमाओं-काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से ऊपर उठकर एक दिव्य जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस संसार में जो कुछ होता है, कदाचित वह माया है, क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ वैसा का वैसा ही विद्यमान है। यहाँ के सारे पात्र वहाँ हैं। इतने संघर्ष के पश्चात जहां धर्मराज युधिष्ठिर पहुँचते हैं, दुर्योधन वहाँ पहले से ही विद्यमान है। इसके पश्चात किसी कर्म अथवा घटना का कोई अर्थ नहीं रहा जाता। भौतिक धरातल पर जो कुछ भी यहाँ घटित हो रहा है, निस्सार है-यह चिंतन कदाचित आरण्यक संस्कृति का ही परिणाम है।
इस सारे विश्लेषण पर यह कहकर आपत्ति की जा सकती है कि इस प्रकार महाभारत को तीन बार कहा और सुना जाता, प्राचीन ग्रंथकारों का एक आख्यान-शिल्प मात्र था-सचमुच ग्रंथ तीन बार सुनाया और सुना नहीं गया था !
वाल्मीकि रामायण के अनुसार नारद ने सर्वप्रथम, राम के जन्म से भी पहले, ऋषि वाल्मीकि को राम का चरित्र सुनाया था ऋषि ने उस चरित्र के विषय में काव्य की रचना की थी; और फिर लव-कुश ने उस कृति का गायन अयोध्या की राजसभा में किया था। तुलसीदास के ‘रामचरित मानस’ में उस कृति की रचना महादेव शिव ने की थी ‘प्रथम महेश रचि मानस राखा’, उन्होंने यह कथा पार्वती को सुनाई थी। उसी कथा को काकभुषुंडी ने गरुण को सुनाया। वही कथा भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य को सुनाई, और अंततः उसी राम कथा को तुलसी के गुरु नरहरिदास ने उन्हें सुनाया और तुलसी ने उस कथा को काव्य-बद्ध किया।
इसी प्रकार अन्य प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथों में से और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। हम देखते हैं कि यह उसकी आख्यान-शिल्प की एक रूढ़ि है कि कथा की रचना करने वाला कृतिकार सीधे-सीधे स्वयं कथा नहीं सुनाता वरन् एक ऐसा आख्यान-शिल्प अंगीकार करता है, जिसमें एक से अधिक कथा-वाचक और श्रोताओं के युगल होते हैं, और स्वयं कृतिकार भी इस कथा का एक पात्र बन जाता है। यह समानता होने के बावजूद यदि हम उनकी तुलना करें, तो हमें कुछ-न-कुछ अंतर दिखाई पड़ता ही है तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार, रामकथा की रचना चाहे महादेव शिव ने की, किंतु जो ग्रंथ हमारे हाथों में है, वह तुलसी का लिखा हुआ ही है। शेष वक्ता और श्रोता उनसे पहले हो चुके हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि तुलसी की रचना में कोई परिवर्तन, संवर्धन अथवा परिवर्धन नहीं हुआ है। वाल्मीकि-रामायण में ऋषि वाल्मीकि को जब नारद ने रामचरित्र सुनाया, उस समय तक पृथ्वी पर राम का अवतार नहीं हुआ था, और वाल्मीकि ने उस चरित्र को काव्य का रूप दिया, जिसे उनके अल्प-वयस्क शिष्यों-लव कुश ने राम की राज्यसभा में सुनाया। इसमें भी किसी संवर्धन अथवा परिवर्तन की संभावना नहीं है, क्योंकि लव-और कुश बालक हैं, अपने गुरू की वाणी सुना रहे हैं, और काव्य-रचना की क्षमता का परिचय उन्होंने नहीं दिया है।
वेदव्यास रचित कृति का नाम ‘जय’ था; और उसे काव्य कहा गया है। उसका सृजन काव्य के ही रूप में हुआ, ‘‘हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान इत्यादि से शरीर-शुद्धि करके पवित्र हो, कुश का आसन बिछा कर बैठे थे। उस समय नियम-पालनपूर्वक शांत-चित्त हो, वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थिति हो, उन्होंने धर्मपूर्वक महाभारत-इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान-दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा।’’(28 तथा 29 के मध्य के श्लोक/1, आदि-पर्व)
हम अनेक बार घटित घटनाओं का एकान्त में स्मरण करते है; अथवा पुरानी घटनाओं की चर्चा करते हैं। किंतु व्यास की यह स्थिति भिन्न है। यह स्मरण अथवा पुनरावलोकन मात्र नहीं है। इसमें व्यास ध्यान-योग में स्थित हैं और ज्ञान-दृष्टि द्वारा धर्मपूर्वक महाभारत-इतिहास के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। यह वस्तुतः रचना का गर्भाधान है। अभी रचना को अभिव्यक्त नहीं किया गया है, न उसे शब्दबद्ध किया गया है, न लिपिबद्ध-किंतु, व्यास ने उसे मन में रच लिया है। वे ब्रह्मा से कहते हैं, ‘‘मैंने संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाभारत की रचना की है। ब्रह्मन ! मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्तवत रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उसके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उसका प्रशस्त रूप प्रकट किया है।’’ (61-63/1, आदिपर्व) और फिर ब्रह्मा के ही परामर्श के अनुसार उन्होंने गणेश से कहा, ‘‘गणनायक ! आप मेरे द्वारा निर्मित इस ‘महाभारत’ ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा। मैंने मन-ही-मन इसकी रचना कर ली है।’’(77/ 1, आदिपर्व)
‘महाभारत’ संबंधी आज की मान्यताओं के अनुसार व्यास द्वारा रचित उस प्रथम रचना का नाम ‘जय’ था; किंतु इस श्लोकों में उसे ‘महाभारत’ ग्रंथ कहा गया है। बहुत संभव है कि यह श्लोक भी बाद के किसी संवर्द्घन का ही अंग हो; क्योंकि ग्रंथ का नाम ‘जय’ से ‘महाभारत’ तो हो सकता है, ‘महाभारत’ से ‘जय’ नहीं हो सकता। फिर भी इतना स्पष्ट है कि वह कृति ‘काव्य’ है। ब्रह्मा कहते हैं, ‘‘तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब यह काव्य नाम से ही प्रसिद्ध होगी।’’ (72/1, आदिपर्व) किंतु यह काव्य, इतिहास पर आधृत है और इसमें वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों का तत्त्व भी सम्मिलित किया गया है। अतः यह इतिहास का आलेख मात्र नहीं है, यह घटनाओं का वर्णन मात्र नहीं है-यह एक काव्य है, जिसकी वेदव्यास ने रचना की है। रचना वे रच चुके हैं, अतः किसी की इच्छा, प्रसन्नता अथवा आवश्यकता के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। यह उन्होंने किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को ध्यान में रख कर किसी अवसर अथवा आवश्यकता विशेष के लिए नहीं रची है। वे किसी से संबोधित नहीं हैं। उन्होंने इसकी रचना स्वांतःसुखाय ही की है। उनके सम्मुख कोई श्रोता नहीं है, केवल उनके लिपिकार अथवा लेखक, गणपति गणेश बैठे हैं। इसलिए इस रचना का कोई तात्कालिक लक्ष्य अथवा उद्देश्य नहीं है। किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को किसी एक विशिष्ट स्थिति से उबारने, किसी समस्या का समाधन करने, अथवा किसी विशिष्ट जीवन-दृष्टि की स्थापना का प्रयास किया गया है।
इस कृति का नाम है ‘जय’। असत्य पर सत्य की जय, अधर्म पर धर्म की जय। क्योंकि इसके विपरीत की स्थापना करने की आवश्यकता किसी और को हो तो हो, कवि को नहीं है। कवि के रूप में व्यास ने भी यही किया। अतः इस दृष्टि से इस मूल रचना ‘जय’ में घटनाओं की दृष्टि से कौरवों तथा पांडवों के युद्ध का वर्णन किया गया होगा, जिसमें पांडवों की विजय का उल्लासपूर्ण चित्रण होगा। इसमें पांडवों की वीरता और उसके गुणों को प्रस्तुत किया गया होगा, ताकि पाठकों के संस्कारों का परिष्कार हो। यह एक कवि की रचना होगी, जिसमें काव्य के गुणों का समावेश नहीं होगा। अतः इसमें घटना की दृष्टि से युद्ध के पश्चात विजयी होकर पांडवों द्वारा प्रजा के पालन और जीवन के सुखों के भोग का चित्रण होगा। क्षत्रिय कार्यों की प्रशंसा होगी। युद्ध-कर्म पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया गया होगा। उसके विषय में संशय नहीं प्रकट किया गया होगा। स्वयं वासुदेव कृष्ण जिस युद्ध की प्रेरणा थे, जिसे वे धर्म-युद्ध मानते थे, जिस युद्ध पांडवों की विजय के लिए वे अर्जुन के सारथि बने थे-उस युद्ध को व्यास ने निरर्थक नहीं माना होगा। यद्यपि ‘महाभारत’ को बाद में आरण्यक संस्कृति का ग्रंथ कहा गया, किंतु ‘जय’ शीर्षक धारण करने वाला काव्य आरण्यक-संस्कृति वाहक नहीं रहा होगा।
महाभारत जैसे युद्ध-काव्य में रूरू और डुडुंभ के वार्तालाप के माध्यम से ‘अहिंसा’ की महत्ता का प्रवेश कराया गया है और रूरू की जिज्ञासा के फलस्वरूप उसे जनमेजय की कथा सुनाई गई है। यह कदाचित् ‘भारत’ इतिहास का आरंभ है। किंतु ‘भारत’ इतिहास की रचना किसी एकान्त स्थान पर बैठकर किसी कवि की अंतर्प्रेरणा तथा आत्म-संतोष के लिए नहीं हुई है। अब ‘जय’ नामक काव्य एक विशिष्ट संदर्भ से जुड़ गया है। काव्य के स्थान पर इतिहास प्रमुख हो गया है। आर्यों और नागों में शत्रुता की चरम स्थिति पहुँच चुकी है। हस्तिनापुर के आर्य सम्राट जनमेजय ने अपनी प्रतिहिंसा में नागों को समूल नष्ट करने का संकल्प किया है। वह एक बड़े जातीय युद्ध के द्वार पर खड़ा है। ऐसे में अपने पूर्वजों का गौरवज्ञान सुनना चाहता है। युद्ध से पहले उनकी वीरता को अनुभव करना चाहता है।
उन घटनाओं के प्रत्यक्ष द्रष्टा तथा काव्य के रूप में उनके स्रष्टा वेदव्यास स्वयं वहाँ विद्यमान हैं। जनमेजय उनसे वह काव्य सुनना चाहता है। उपर्युक्त अवसर पर उसे सुनने का उद्देश्य मात्र रसास्वादन नहीं है। बागों के विरूद्ध इस युद्ध का औचित्य सिद्ध करने तथा अपने लिए युद्धोन्माद का बल पाने के लिए वह ‘जय’ काव्य सुनना चाहता है।
किंतु वेदव्यास के लिए जनमेजय और नागों का युद्ध, धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं था। वह जातीय युद्ध था, जिसमें एक जाति प्रतिशोध के लिए प्रति-हिंसावश अपने शस्त्र बल से दूसरी जाति को मिटा देना चाहती थी। निश्चित रूप से वेदव्यास, एक ओर आर्य सम्राट जनमेजय का उत्साह खंडित नहीं करना चाहते होंगे और दूसरी ओर वे युद्धोन्माद की अग्नि को प्रचंड करना भी श्रेय़स्कर नहीं मानते होंगे। उन्होंने कौरवों और पांडवों के युद्ध में धर्म की विजय का उद्घोष किया था। यदि संभव होता तो स्वयं वासुदेव कृष्ण और कृष्ण द्धैपायन व्यास युद्ध के स्थान पर धर्माधत संधि ही चाहते। दुर्योधन ने उसे संभव नहीं होने दिया; आर्यों तथा नागों में प्रश्न धर्म और अधर्म पक्ष का नहीं था। यहाँ भेद जाति का था और व्यक्ति की प्रतिहिंसा जाति का द्वेष बन गई थी। दोनों जातियाँ प्रतिशोध का भाव त्याग कर क्षमा और उदारता के आधार पर संधि कर सकती थीं। इस समय वेदव्यास ने आर्यों और नागों में किसी सम्मानजनक संधि की ही कामना की होगी।
उन्होंने अपने शिष्य से कहा, ‘‘वैशम्पायन ! पूर्वकाल में कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, जिसे तुम मुझ से सुन चुके हो, यह सब इन राजा जनमेजय को सुनाओ।’’ (22/60, आदिपर्व)
महाभारत के वर्णन के अनुसार, ‘‘उस समय गुरूदेव व्यास जी की आशा पाकर विप्रवर वैशम्पायन ने राजा जनमेजय, सभासदगण तथा अन्य सब भ्रूपालों से कौरव-पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी और उसका सर्वनाश हुआ-वह सब पुरातन इतिहास कहना आरंभ किया।’’(23-24/60, आदिपर्व)
अब यह इतिहास है-‘भारत’ इतिहास ! इसे काव्य नहीं कहा गया। इस इतिहास के मूल में फूट की चर्चा है, फूट के कारण युद्ध और युद्ध के कारण सर्वनाश का उल्लेख है। निश्चित रूप से सर्वनाश करने वाले ‘युद्ध’ का समर्थन न वेदव्यास करेंगे, न उनके शिष्य वैशम्पायन; किंतु एक क्षत्रिय राजा के सम्मुख वे युद्ध का निषेध भी नहीं कर सकते। अतः युद्ध के परिणामों के प्रति सावधान करने के लिए युद्धोन्मुख राजा ही सर्वोत्तम पात्र है। वैशम्पायन कहते हैं, ‘‘जनमेजय ! तुम इस महाभारत कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो और मुझे यह कथा उपलब्ध है, तथा श्रीगुरूजी के मुखारविन्द से मुझे यह आदेश भी मिल गया है कि मैं तुम्हें यह कथा सुनाऊं। इससे मेरे मन को बड़ा उत्साह प्राप्त होता है। राजन् ! जिस प्रकार कौरवों और पांडवों में फूट पड़ी-वह प्रसंग सुनो। राज्य के लिए जो जुआ खेला गया, उससे उनमें फूट हुई और उसी के कारण पांडवों का वनवास हुआ। भरतश्रेष्ठ ! फिर जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत युद्ध हु्आ, वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुमसे कहता हूँ, सुनो।’’(3-5/61 आदिपर्व)
इस उक्ति में वैशम्पायन बहुत सावधान हैं। वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि युद्ध का मूल कारण राज्य है, उस राज्य के कारण फूट पड़ी और युद्ध हुआ; किंतु युद्ध से समस्या का समाधान हुआ या नहीं, सर्वनाश अवश्य हुआ। वैशम्पायन द्वारा सुनाए जा रहे ‘भारत’ में युद्ध को क्षत्रिय के काम्य लक्ष्य के स्थान पर विनाशकारी कर्म के रूप में रेखांकित किया जा रहा है। यहीं से महाभारत में ‘युद्ध’ को किसी समस्या के समाधान के रूप में देखने के प्रति संशय का भाव उत्पन्न हुआ होगा। यदि युद्ध को समस्याओं के समाधान के रूप में स्वीकार किया जाता तो आर्यों और नागों में भंयकर युद्ध होता, जिसमें संभवतः आर्यों की भी बहुत भारी क्षति होती; किंतु नागों का तो सर्वनाश होकर ही रहता। इसलिए सारे चिन्तकों तथा मनीषियों के द्वारा ‘युद्ध’ के स्थान पर राजनीतिक समाधान को ही वरीयता दी गई। जनमेजय ने आस्तीक को वरदान दिया। तक्षक को क्षमा किया गया; और नागों को सुखपूर्वक रहने की अनुमति दी गई।
दृष्टिकोण के इस परिवर्तन का प्रभाव कथा की रूपरेखा पर भी पड़ा होगा। वैशम्पायन की कथा में युधिष्ठिर को युद्ध के लिए और भी अनिच्छुक दिखाया गया होगा। युधिष्ठिर में आनृशंसता के भाव की वृद्धि की गई होगी और सबसे बड़ी बात है विजय के पश्चात भी निराशा, दुख तथा विषाद का हाथ लगना दिखाया गया होगा, जिससे युद्ध के प्रति उत्साह न बढ़े और युद्ध को विजय, उल्लास तथा सुख-भोग का सरल मार्ग न माना जाए। संभव है कि युद्धोपरांत निराशा तथा हताशा के सारे प्रसंग इसी अवसर पर या तो रचकर जोड़े गए हों; अथवा उन्हें रेखांकित कर विषाद का रंग गाढ़ा किया गया हो।
यहां एक आपत्ति यह की जा सकती है कि महाभारत के वर्णन के अनुसार, जनमेजय द्वारा यज्ञ रोक दिए जाने तथा तक्षक को क्षमा कर दिए जाने के पश्चात वेदव्यास का पदार्पण होता है। ऐसी स्थिति में यह कैसे माना जा सकता है कि यह प्रभाव वैशम्पायन द्वारा सुनाई गई कथा का था ?
पहली बात तो यही है कि तर्क-संगत निष्कर्ष निकालने के लिए पुराण कथाओं की शिथिलता को भी ध्यान में रखना चहिए। दूसरी बात यह है कि ‘महाभारत’ में भी यह स्पष्ट है कि वेदव्यास नाग-यज्ञ में ही पधारे थे। ‘महाभारत’ कथा सुनने के अंत तक आस्तीक भी वहीं था और कथा की समाप्ति के पश्चात ही यज्ञ को पूर्णतः समाप्त घोषित किया गया था और जनमेजय तक्षशिला से हस्तिनापुर लौटा था। न तो वेदव्यास टहलते हुए तक्षशिला पहुँचे थे और न ही वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि जनमेजय नाग-यज्ञ कर रहा है। यदि आस्तीक ने अपने उद्यम द्वारा यज्ञ को समाप्त करवा दिया होता तो जनमेजय महाभारत की कथा सुनने के लिए वहां बैठा नहीं रहता। वस्तुतः महाभारत की कथा जनमेजय को यज्ञ के मध्य ही सुनाई गई, जिससे उसकी समझ में आया होगा कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं होता।
वैशम्पायन द्वारा सुनाए गए इस ‘भारत’ इतिहास में निश्चय ही हिंसा तथा प्रतिहिंसा के अवमूल्यन का प्रयत्न किया गया होगा और अहिंसा की महिमा को स्थापित किया गया होगा।
महाभारत का तृतीय आरंभ जिस परिवेश में हुआ है, उसका वर्णन स्वयं महाभारत में इस प्रकार हैः ‘‘एक समय की बात है। नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के बारह वर्षों से चलते रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुख-पूर्वक बैठे थे,. सूत-कुल को आनन्दित करने वाले लोमहर्षण-पुत्र उग्रश्रवा सौति स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथा-वाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवा जी को उनसे चित्र-विचित्र कथाएँ सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया।’’(1-3/1, आदिपर्व)
इस वक्तव्य में अनेक बातें ध्यातव्य हैं। प्रथम तो यह कि नैमिषारण्य में कुलपति शौनक का आश्रम है, यहाँ सांसारिक चर्चाएं नहीं होतीं। दूसरे जो श्रोता वहां एकत्रित हैं वे ब्रह्मर्षि हैं। उनके जीवन का लक्ष्य ब्रह्म-प्राप्ति है। फिर वे लोग इस समय कुलपति शौनक के बारह वर्षों तक चलने वाले सत्र में पधारे हैं। निश्चित रूप से इस समय उनके मन और भी अधिक एकाग्र हैं तथा अपने लक्ष्य के प्रति और भी अनुकूलित हैं। इस समय वे कोई साधारण काव्य नहीं सुनना चाहते होंगे, न उनकी इच्छा युद्ध तथा शांति की समस्याओं पर वक्तव्य सुनने की होगी। वे अवकाश के क्षणों में हैं, अतः संभव है, वे कुछ बौधिक मनोरंजन भी चाहती हों।
सौति उग्रश्रवा उन्हीं से पूछते हैं कि वे क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि श्रव्य-काव्य तथा कथावाचन की परंपरा में वाचन में भी अधिक महत्त्वपूर्ण श्रोता का व्यक्तित्व, उसकी मनःस्थिति तथा उसकी तत्कालीन आवश्यकता है। उग्रश्रवा पूछते हैं, ‘‘इस समय आप सभी स्नान, संध्या-वंदन, जप तथा अग्निहोत्र आदि करके, शुद्ध हो, अपने-अपने आसन पर स्वस्थचित से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं ? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न-भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं स्मृतियों का पवित्र इतिहास।’’ (15-16/1, आदिपर्व)
ऋषियों ने अपनी रूचि प्रकट करते हुए कहा, ‘‘उग्रश्रवा जी ! परमर्षि द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास-रूप पुराण का वर्णन किया है, और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने-अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक-एक पद, वाक्य एवं, पर्व, विचित्र शब्द-विन्यास और रमणीय अर्थ से पूर्ण है, जिसमें आत्मा-परमात्मा के सूक्ष्म-स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी, ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली, पदों-वाक्यों की व्युत्पत्ति से मुक्त, सब शस्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनके समर्थित जो अद्भुतकर्म व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्यस्वरूपा है। पाप और भय का नाश करने वाली है ।’’(17-21/ 1, आदिपर्व)
स्पष्टताः इसमें इस कृति को ‘इतिहास’ कहा गया है। वस्तुतः ‘जय’ काव्य के पश्चात यह कृति ‘भारत’ नामक इतिहास हो गई-इसमें कोई संशय नहीं है; किंतु यह इतिहास, साधारण इतिहास नहीं है। इसमें अन्य अनेक गुणों के साथ-साथ ‘आत्मा-परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियाँ भरी हुई हैं। उग्रश्रवा के श्रोताओं की सबसे अधिक रूचि ‘आत्मा-परमात्मा के स्वरूप’ और उनके अनुभव की युक्तियों में ही हो सकती है। ‘‘उग्रश्रवा एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम तथा यथार्थ कथा कहने लगे।’’ (8/1, आदिपर्व) मुझे लगता है कि इस तीसरे वाचन ने इस कृति को ‘भारत’ से ‘महाभारत’ बना दिया। इसमें या तो इतिहास रह गया था अध्यात्म। उग्रश्रवा ने कहा, ‘‘शौनक जी ! आपके इस सतसंग सत्र में यह जो उत्तम इतिहास ‘महाभारत’ सुना रहा हूँ, यही जनमेजय के सत्र-यज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशम्पायन जी के द्वारा भी वर्णित किया गया था। (33/1, आदिपर्व) बहुत संभव है कि कुशल वक्ता और कथावाचक उग्रश्रवा ने इसमें अपनी दृष्टि के अनुकूल अनेक ऐतिहासिक-पौराणिक कथाएं जोड़ी हों। उन्होंने कहा, ‘‘जैसे भोजन किए बिना शरीर-निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इतिहास का आश्रय लिए बिना, पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है।’’(33/ 1, आदिपर्व) किंतु यह इतिहास उग्रश्रवा के लिए साध्य नहीं था, वह मात्र साधन ही था। संभवताः संवर्धन के इसी चरण में महाभारत की कथा मर्त्यलोक से स्वर्ग-लोक तक पहुँच गई। युधिष्ठिर आनृशंसता से भी आगे बढ़कर सम-दृष्टि को प्राप्त हो चुका था, जो अपने भाइयों को स्वर्गारोहण के समय गिरते हुए देखकर भी विचलित नहीं होता तथा अपने साथ आए हुए कुत्ते का त्याग कर स्वर्ग भी प्राप्त नहीं करना चाहता। यह उद्देश्य कदाचित आध्यात्मिक चिंतन से उद्भूत है, वह भौतिक भोगों की निरर्थकता तथा अधिकार के लिए लड़े गए युद्धों के लिए ही हिंसा की निस्सारता चित्रित कर, मनुष्य को अपनी सीमाओं-काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से ऊपर उठकर एक दिव्य जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस संसार में जो कुछ होता है, कदाचित वह माया है, क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ वैसा का वैसा ही विद्यमान है। यहाँ के सारे पात्र वहाँ हैं। इतने संघर्ष के पश्चात जहां धर्मराज युधिष्ठिर पहुँचते हैं, दुर्योधन वहाँ पहले से ही विद्यमान है। इसके पश्चात किसी कर्म अथवा घटना का कोई अर्थ नहीं रहा जाता। भौतिक धरातल पर जो कुछ भी यहाँ घटित हो रहा है, निस्सार है-यह चिंतन कदाचित आरण्यक संस्कृति का ही परिणाम है।
इस सारे विश्लेषण पर यह कहकर आपत्ति की जा सकती है कि इस प्रकार महाभारत को तीन बार कहा और सुना जाता, प्राचीन ग्रंथकारों का एक आख्यान-शिल्प मात्र था-सचमुच ग्रंथ तीन बार सुनाया और सुना नहीं गया था !
वाल्मीकि रामायण के अनुसार नारद ने सर्वप्रथम, राम के जन्म से भी पहले, ऋषि वाल्मीकि को राम का चरित्र सुनाया था ऋषि ने उस चरित्र के विषय में काव्य की रचना की थी; और फिर लव-कुश ने उस कृति का गायन अयोध्या की राजसभा में किया था। तुलसीदास के ‘रामचरित मानस’ में उस कृति की रचना महादेव शिव ने की थी ‘प्रथम महेश रचि मानस राखा’, उन्होंने यह कथा पार्वती को सुनाई थी। उसी कथा को काकभुषुंडी ने गरुण को सुनाया। वही कथा भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य को सुनाई, और अंततः उसी राम कथा को तुलसी के गुरु नरहरिदास ने उन्हें सुनाया और तुलसी ने उस कथा को काव्य-बद्ध किया।
इसी प्रकार अन्य प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथों में से और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। हम देखते हैं कि यह उसकी आख्यान-शिल्प की एक रूढ़ि है कि कथा की रचना करने वाला कृतिकार सीधे-सीधे स्वयं कथा नहीं सुनाता वरन् एक ऐसा आख्यान-शिल्प अंगीकार करता है, जिसमें एक से अधिक कथा-वाचक और श्रोताओं के युगल होते हैं, और स्वयं कृतिकार भी इस कथा का एक पात्र बन जाता है। यह समानता होने के बावजूद यदि हम उनकी तुलना करें, तो हमें कुछ-न-कुछ अंतर दिखाई पड़ता ही है तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार, रामकथा की रचना चाहे महादेव शिव ने की, किंतु जो ग्रंथ हमारे हाथों में है, वह तुलसी का लिखा हुआ ही है। शेष वक्ता और श्रोता उनसे पहले हो चुके हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि तुलसी की रचना में कोई परिवर्तन, संवर्धन अथवा परिवर्धन नहीं हुआ है। वाल्मीकि-रामायण में ऋषि वाल्मीकि को जब नारद ने रामचरित्र सुनाया, उस समय तक पृथ्वी पर राम का अवतार नहीं हुआ था, और वाल्मीकि ने उस चरित्र को काव्य का रूप दिया, जिसे उनके अल्प-वयस्क शिष्यों-लव कुश ने राम की राज्यसभा में सुनाया। इसमें भी किसी संवर्धन अथवा परिवर्तन की संभावना नहीं है, क्योंकि लव-और कुश बालक हैं, अपने गुरू की वाणी सुना रहे हैं, और काव्य-रचना की क्षमता का परिचय उन्होंने नहीं दिया है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i