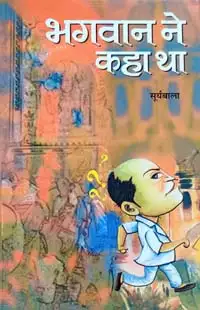|
कहानी संग्रह >> पाँच लम्बी कहानियाँ पाँच लम्बी कहानियाँसूर्यबाला
|
412 पाठक हैं |
|||||||
मनोवैज्ञानिक धरातल पर मानसिक अंतर्दशाओं का अभिव्यंजन.....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
डॉ.सूर्यबाला की ये पांच लम्बी कहानियां मनोवौज्ञानिक धरातल पर मानसिक
अंतर्दशाओं का अभिव्यंजन करती हैं। ‘गृह प्रवेश’ आर्थिक दबाव
में अनचाहे समझौतों की विवशता का आख्यान है। भुक्खड़ की औलाद एक शिक्षित,
किन्तु बेरोजगार व्यक्ति की करुण त्रासदी है, जो पारिवारिक ममता और मानवीय
संवेदना को तिलांजलि देकर भी जीवन की दारुण परिणितों से बच नहीं पाता।
‘मानसी’ में किशोर मन की उस निगूढ़ भावानुभूति का
चित्रण है,
जो नीति, उम्र और आचार-संहिता के परे आजीवन अभिन्न सहचरी बनी रहती है।
‘मटियाला तीतर’ एक अशिक्षित, किन्तु बुद्धिमान और
स्वाभिमान
बालक का आख्यान है, जो आर्थिक विपन्नता में भी पारिवारिक प्रेम,
आत्माभिमान और मुक्त जीवन-शैली को नहीं भूल पाता। तथाकथित सभ्य परिवार के
छद्म से आहत होकर वह जीवन से ही विमुख हो जाता है। ‘अनाम लमहों
के
नाम’ में मध्य वर्गीय संकुचित मनोवृत्ति, स्वार्थपरता,
संवेदनाशून्यता, अमानवीय अवसरवादिता के चित्रण के साथ नई पीढ़ी पर उसके
कुप्रभावों का रेखांकन है।
इन कहानियों में संस्मरणात्मक और रेखाचित्रात्मक संस्पर्श होने के कारण अनुभूति की प्रामाणिकता निखर गई है। ये कहानियाँ जहाँ मानव मन की संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अख्यान प्रस्तुत करती हैं वहीं विभिन्न अनुषंगों से युग व्यापी मूल्यहीनता, भ्रष्टता, सांप्रदायिक संकीर्णता, आर्थिक विपन्नता, मानवीय संबंधों की कृत्रिमता, अमानवीय स्वार्थपरता जैसी पारिवेशिक विशेषताओं का प्रभावी चित्रण करती हैं। ये कहानियां अपनी वस्तु और शिल्पगत नवता में संवेदनात्मक चेतना से सम्पन्न अभिनव पाठकीय संस्कार की तलाश करती प्रतीत होती हैं।
इन कहानियों में संस्मरणात्मक और रेखाचित्रात्मक संस्पर्श होने के कारण अनुभूति की प्रामाणिकता निखर गई है। ये कहानियाँ जहाँ मानव मन की संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अख्यान प्रस्तुत करती हैं वहीं विभिन्न अनुषंगों से युग व्यापी मूल्यहीनता, भ्रष्टता, सांप्रदायिक संकीर्णता, आर्थिक विपन्नता, मानवीय संबंधों की कृत्रिमता, अमानवीय स्वार्थपरता जैसी पारिवेशिक विशेषताओं का प्रभावी चित्रण करती हैं। ये कहानियां अपनी वस्तु और शिल्पगत नवता में संवेदनात्मक चेतना से सम्पन्न अभिनव पाठकीय संस्कार की तलाश करती प्रतीत होती हैं।
रामजी तिवारी
तेरा, तुझको...
बगल में बैठी वह –
मुझसे निरासक्त
मेरी कहानी पढ़ती गई।
पढ़ते हुए उसी तरह हँसी
और रोई-
जैसे मैं उस कहानी को रचते समय
फिर मेरी तरफ पलटी-
‘अच्छा मैडम !
मेरे साथ तो इस कहानी जैसा कुछ घटा नहीं-
फिर भी ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि
नहीं, घटा है सबकुछ मेरे साथ भी
यहाँ मैं हूँ, यहाँ भी...और यहाँ भी...
तृप्ति भी, भूख भी...
भूख भी, तृप्ति भी...
अचानक ही जैसे-
अपने से मुलाकात हुई हो’....
ऐसे हर मुलाकाती को –
जिनकी पारस संवेदना के
स्पर्श की प्रतीक्षा
हर रचना को रहती है।
बगल में बैठी वह –
मुझसे निरासक्त
मेरी कहानी पढ़ती गई।
पढ़ते हुए उसी तरह हँसी
और रोई-
जैसे मैं उस कहानी को रचते समय
फिर मेरी तरफ पलटी-
‘अच्छा मैडम !
मेरे साथ तो इस कहानी जैसा कुछ घटा नहीं-
फिर भी ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि
नहीं, घटा है सबकुछ मेरे साथ भी
यहाँ मैं हूँ, यहाँ भी...और यहाँ भी...
तृप्ति भी, भूख भी...
भूख भी, तृप्ति भी...
अचानक ही जैसे-
अपने से मुलाकात हुई हो’....
ऐसे हर मुलाकाती को –
जिनकी पारस संवेदना के
स्पर्श की प्रतीक्षा
हर रचना को रहती है।
भूमिका
अंजलि का यह जल....
वह तन्मय भाव से प्रश्नों के उत्तर लिखते-लिखते अचानक पूछ बैठी थी,
‘‘अच्छा ! लिखती कैसे हैं आप ?’’
‘‘एक अपराध की तरह।’’ हकबकी, भौंचक वह मेरा मुँह देखती रह गई थी। निश्चित रूप से यह उत्तर उसकी अपेक्षाओं से बहुत नीचे था। किसी अप्रतिम, विलक्षण की जगह, मामूलीपन की निरीहता में डूबा हुआ; लेकिन फिर जैसे आपसे आप उसकी समझ में आता गया कि सत्य की साख उसकी प्रामाणिकता, उसकी सच्चाई में है – वह कितना कड़ुआ, कितना मीठा या कितना करुण है, इसमें नहीं।
तो मेरा लिखना पिछले अट्ठाईस वर्षों से चले आते एक अपराध भाव, पछतावों और बेचैनियों का सिलसिला है – अनवरत, अविकल – इसी से शायद टूटा और छूटा भी नहीं। यह एक बहुत बड़ी राहत है और अगले वर्षों, अगली यात्राओं का पाथेय भी।
इस अपराध भाववाली बात को शायद थोड़ा और खोलने की जरूरत है। तो सीधे-सीधे, मैं अक्सर यह सोचती हूँ कि किसी रचनाकार (पुरुष या स्त्री) का उसके कुटुंब, परिवार के छोटे-छोटे सुख, दु:ख भरे लमहों या दैनंदिन कार्यकलापों में कितना साझा होता है ? वह कितने सुख सहेज पाता है, कितने दु:ख बाँट पाता है। अनचाहे कितने आत्मीय फलों से वंचित रहता भी है, करता भी है...क्या उसका लेखन कहीं उसके घर-परिवार की अपेक्षाएँ पूरी करने में बाधा नहीं बनता ? तब क्या लेखन से न्याय करनेवाला जीवन के प्रति अन्याय न सही, ज्यादती का अपराधी माना जाए ? घुनकर, जमकर लिखनेवाले महारथी अकसर डंके की चोट पर ऐसी घोषणाएँ करते नजर आते हैं कि जीवन और लेखन दोनों एक साथ नहीं सँभल सकते। यह खाला का घर नहीं है – ‘सीस उतारे भुँइ धरे तब पईठे घर माहि’ – इतना ही क्यों, सीधे-सीधे ‘जो घर फूँकै अपना’...वही चल पाएगा इस राह पर और यह राह भी कैसी कि ‘इक आग का दरिया है’ और...तिल-तिल कर होम करते जाने का दूसरा नाम...ऐसे वक्तव्यों में बहुत सच्चाई है, यह तो कम-से-कम हर लिखनेवाला जानता है। मुझे तो खास तौर से दुधारी तलवार की तरह बेधते हैं ये निष्कर्ष। गहराते द्वंद्व बेचैन करते हैं कि तब क्या दोतरफा अन्याय कर रही हूँ मैं ? न जीवन से न्याय, न लेखन से ? एक नकली, झूठा और फरेबी जीवन जी रही हूँ मैं ! (और शायद वैसा ही लेखन भी) विभाजित रेखाओं में कटा-फटा अस्तित्व, व्यक्तित्व। द्वंद्व, दुविधाओं का एक उलझा-पुलझा गुल्लर। मैं समय तो चुराता हूँ परिवार का, लेकिन यश, कीर्ति, प्रसिद्धि मेरी अपनी। मेरे परिवार को क्या हासिल है इससे ?
लेकिन निसर्ग और जीवन के साथ एक बड़ी विलक्षण बात यह है कि सच होने के बावजूद किसी भी सत्य को अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता। हम अपने सत्यों की तालाश और निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं। रचनात्मकता का एक पक्ष शायद ऐसे ही सत्यों का सृजन करना है भी; हमें सुस्थिर और सुचित्त करना भी। अकसर तूफानी झंझावातों के थमने के बाद जिस तरह एक शांतिमयी शीतलता की अनुभूति होती है, कुछ-कुछ वैसा ही द्वन्द्वों के ऊहापोहों से उबरने के बाद भी होता है। वेगवती लहरों के बीच से अंजलि में उठाए शीतल जल-सा पिघलती, मचलती लहरों में प्रवहमान जल का अपना सच होता है। अंजलि में समाए जल का अपना।
अंजलि का यही जल मेरा सच है। मैं इससे तृप्त हूँ। यह तृप्ति लेखन की नहीं है, जीवन के प्राप्य और प्राप्ति के सामंजस्य की है। मुझे नहीं लगता कि जीवन खोकर लेखन या लेखन छोड़कर ही जीवन को समग्रत: पाया जा सकता है। यथार्थ में दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। जो जीवन में अतल तक नहीं डूबा, उसके लेखन में क्या उतराएगा....और जीवन के ऊपरी तमाशबीनी नहीं, गहरी मार्मिकता चाहिए लेखक को। तब शायद लेखन का विरोध जीवन से नहीं, लेखन कर्म से जुड़ी विरूपताओं और आपाधापियों से है। लेखन अब सुख नहीं, प्रतिस्पर्द्धी महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बन गया है। लोग कहते हैं तो इसमें बुरा क्या है। यह तो हमेशा से हर देश के साहित्य और लेखन के साथ होता आया है। प्रतिस्पर्धा बेहतर लेखन की प्रेरणा बनती है, लेखन में चुनौतियों को स्वीकारने की स्फूर्ति और ऊर्जा भरती है, साहित्य को समद्ध करती है।
लेकिन मुझे तो लगता है, कितना अच्छा हुआ जो कबीर, तुलसी और सूर के समय में ऐसी चुनौतियाँ और प्रेरणाएँ नहीं थीं। मीरा साहित्य-सृजन के इन उपादानों की बेचैनियों से मुक्त थीं। स्पर्द्धा और होड़ा-होड़ी रीतिकालीन स्थितियों की माँगें थीं, मानसिकता थीं, जिसका प्रभाव समूचे रीति काव्य में दृष्टिगत होता है। वहाँ उपादान बहुत हैं, चाव भी; भाव कम। विश्व के उत्कृष्टम ग्रन्थों की रचना ऐसी प्रेरणाओं से विहीन, उद्दीपनहीन स्थितियों में ही होती रही है। प्राय: प्रतिस्पर्द्धी और तथाकथित चुनौतियों से ठस्समठस्स माहौल में, मात्रा में कहीं ज्यादा, लाउड और सामयिक मुद्दों की धार में भरपूर डुबकी लगानेवाला ट्रेंडी लेखन भले हो जाए, आत्मा में पैठकर उसमें उजास भरनेवाला लेखन अपेक्षाकृत कम हो पाता है। होता भी है तो ऊँची उछाल भरने की असमर्थता की वजह से ऊपर नहीं आ पाता। वर्चस्व, सामाजिक, राजनीतिक विरूपताओं पर उतने ही विरूप प्रहार करनेवाली दबंगई और पूर्वाग्रही निष्कर्षों का ही होता है। दुर्द्धर्ष वैचारिकता तथा प्रतिमा का ऐसा एकांगी इस्तेमाल अकसर देखने को मिल जाता है। वहाँ दृष्टि के विस्तार को बलात् समेटा जा सकता है, पक्षी के पंख काटकर पिंजरे में बंद कर लेने की तरह। अपनी ही प्रतिभा, पारदर्शिता और वैचारिक क्षमता के पंख कतरने की यह प्रवृत्ति काफी कुछ मानव बमों की तरह सर्वग्रामी और आत्मघाती एक साथ होती है।
क्या आज के माहौल में किसी ऐसे रचनाकार की कल्पना की जा सकती है जो अपने आपको चारों तरफ से घोर व्यावयायिक दबावों से मुक्त रखकर लेखन कर सके ? व्यावसायिकता से मेरा आशय समाज में नहीं, लेखन के क्षेत्र में व्याप्त निरंकुश व्यावसायिक स्थितियों से है। हर लेखक के चेतन अवचेतन में कमोबेश इन व्यापारों का व्यामोह पलता ही है। पुरस्कारों, अनुदानों, पुस्तक मेलों और लोकार्पणों, उद्घाटनों को लेकर जो हास्यास्पद दौड़े लगती हैं, समय और शक्ति का जो अपव्यय होता है, जो हडबोंग मचती है उसे देखकर यही लगता है कि आज सफल लेखक के लिए सफल व्यवसायी होना ज्यादा जरूरी है। अब बाजार की माँग की पूर्ति तो होनी ही है, इसलिए देखते-देखते एक लेखक की शख्सियत का बहुतांश व्यवसायी होता चला जाता है। यहाँ तक कि बाकी रोजगारियों के तो कुछ असूल होते भी हों, लेकिन यह त्वरित उपलब्धि का उतावला व्यवसायी इस ‘धंधे’ में सबकुछ ‘जायज’ कर चलने का अभ्यस्त हो जाता है।
लोग चाहे तो कहें, लेकिन मुझे लगता है, लेखक सिर्फ उतना भर ही नहीं है जितना वह कागज पर उतारता है, वह उससे बहुत ज्यादा है। कागज पर उतरने-उतराने के बाद बचे इस लेखक-शेष का भी, नीति की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, वृत्ति, प्रवृत्ति और संवेदना से उतना ही समृद्ध भरपूर होना है जितना वह कागजों पर उतारता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अपनी सारी संवेदना कागजों पर ही खर्च कर मुक्त हो जाए और एक मामूली इन्सान भर भी इनसान न रह जाए। क्या लेखन से बड़ी महत्त्वाकांक्षा अपने अंदर के इनसान को बचाए रखने की नहीं चाहिए ? कागज पर उतरने और जीवन में विचरनेवाले लेखक के बीच उभयनिष्ठ रंग-रेखाएँ नहीं होंगी तो पढ़नेवाले अपना विश्वास कहाँ रोपेंगे ? वे अपने लिए आधार और आलंबन कहाँ ढूढ़ेंगे ? मुझे मालूम है, यह देश-विदेश के सैकड़ों ऐसे कलाकारों, साहित्यकारों के जीवन और लेखन के बीच की परस्पर प्रतिरोधी मिसालें दी जा सकती हैं। यह भी कि बावजूद इन विपरीत गुणों के उनकी कृतियाँ अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कीर्तिमान बना चुकी हैं, किन कीर्तिमानों का गणित हमेशा जीवन का कुतुबनुमा नहीं हुआ करता। मात्र अति बौद्धिकता में ही अथ और इति को प्राप्त होनेवाली कृतियों से जीवन-दिशाएँ नहीं बदला करतीं। उन्हें असल और निष्पक्ष चाहिए होता है और ये ही दोनों बुरी तरह उलझते-पुलझते गए हैं इस पूरी शताब्दी में। उलझाव का संक्रमण कर समर्थ रहा है यह....और सुलझानेवाली शक्तियाँ लगातार क्षरित होती रही हैं। अन्यथा सारी इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजिकल मारामारी के बावजूद आदमी आज ज्यादा सहूलियत से जिंदा रह पाता। संवेदना की जो विरासतें कला और साहित्य के माध्यम से उसे मिल सकती थीं, नहीं मिल पाईं।
इसलिए अपने अपराध-बोध को बहुत गैर जरूरी नहीं मान पाती मैं; क्योंकि है तो यह भी किसी संवेदना के घनत्व के बीच से ही उपजा। तो पहली आश्वस्ति तो यही कि कम-से-कम, संवेदना की यह संजीवनी, जिलाए रखेगी मेरे अंदर के लेखक और आदमी को भी। मुझे सोचने पर विवश भी करती रहेगी कि अपने जीवन और लेखन की विभाजित भूमिकाओं में मैं कितनी खरी उतर पा रही हूँ, कितनी ईमानदारी बरत रही हूँ ? अपने ‘देय’ के प्रति कितनी सजग और सचेष्ट हूँ ? दुकान छोटी ही सही, माल में मिलावटी घालमेल तो नहीं ? एक बात और, माल कितना भी
भरा हो, लेकिन बेचना वह है जिसकी लोगों को आज जरूरत है।
‘पाँच लंबी कहानियाँ’ इस जरूरत को थोड़ा-बहुत पूरा करती हैं, इस संतोष के साथ –
‘‘एक अपराध की तरह।’’ हकबकी, भौंचक वह मेरा मुँह देखती रह गई थी। निश्चित रूप से यह उत्तर उसकी अपेक्षाओं से बहुत नीचे था। किसी अप्रतिम, विलक्षण की जगह, मामूलीपन की निरीहता में डूबा हुआ; लेकिन फिर जैसे आपसे आप उसकी समझ में आता गया कि सत्य की साख उसकी प्रामाणिकता, उसकी सच्चाई में है – वह कितना कड़ुआ, कितना मीठा या कितना करुण है, इसमें नहीं।
तो मेरा लिखना पिछले अट्ठाईस वर्षों से चले आते एक अपराध भाव, पछतावों और बेचैनियों का सिलसिला है – अनवरत, अविकल – इसी से शायद टूटा और छूटा भी नहीं। यह एक बहुत बड़ी राहत है और अगले वर्षों, अगली यात्राओं का पाथेय भी।
इस अपराध भाववाली बात को शायद थोड़ा और खोलने की जरूरत है। तो सीधे-सीधे, मैं अक्सर यह सोचती हूँ कि किसी रचनाकार (पुरुष या स्त्री) का उसके कुटुंब, परिवार के छोटे-छोटे सुख, दु:ख भरे लमहों या दैनंदिन कार्यकलापों में कितना साझा होता है ? वह कितने सुख सहेज पाता है, कितने दु:ख बाँट पाता है। अनचाहे कितने आत्मीय फलों से वंचित रहता भी है, करता भी है...क्या उसका लेखन कहीं उसके घर-परिवार की अपेक्षाएँ पूरी करने में बाधा नहीं बनता ? तब क्या लेखन से न्याय करनेवाला जीवन के प्रति अन्याय न सही, ज्यादती का अपराधी माना जाए ? घुनकर, जमकर लिखनेवाले महारथी अकसर डंके की चोट पर ऐसी घोषणाएँ करते नजर आते हैं कि जीवन और लेखन दोनों एक साथ नहीं सँभल सकते। यह खाला का घर नहीं है – ‘सीस उतारे भुँइ धरे तब पईठे घर माहि’ – इतना ही क्यों, सीधे-सीधे ‘जो घर फूँकै अपना’...वही चल पाएगा इस राह पर और यह राह भी कैसी कि ‘इक आग का दरिया है’ और...तिल-तिल कर होम करते जाने का दूसरा नाम...ऐसे वक्तव्यों में बहुत सच्चाई है, यह तो कम-से-कम हर लिखनेवाला जानता है। मुझे तो खास तौर से दुधारी तलवार की तरह बेधते हैं ये निष्कर्ष। गहराते द्वंद्व बेचैन करते हैं कि तब क्या दोतरफा अन्याय कर रही हूँ मैं ? न जीवन से न्याय, न लेखन से ? एक नकली, झूठा और फरेबी जीवन जी रही हूँ मैं ! (और शायद वैसा ही लेखन भी) विभाजित रेखाओं में कटा-फटा अस्तित्व, व्यक्तित्व। द्वंद्व, दुविधाओं का एक उलझा-पुलझा गुल्लर। मैं समय तो चुराता हूँ परिवार का, लेकिन यश, कीर्ति, प्रसिद्धि मेरी अपनी। मेरे परिवार को क्या हासिल है इससे ?
लेकिन निसर्ग और जीवन के साथ एक बड़ी विलक्षण बात यह है कि सच होने के बावजूद किसी भी सत्य को अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता। हम अपने सत्यों की तालाश और निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं। रचनात्मकता का एक पक्ष शायद ऐसे ही सत्यों का सृजन करना है भी; हमें सुस्थिर और सुचित्त करना भी। अकसर तूफानी झंझावातों के थमने के बाद जिस तरह एक शांतिमयी शीतलता की अनुभूति होती है, कुछ-कुछ वैसा ही द्वन्द्वों के ऊहापोहों से उबरने के बाद भी होता है। वेगवती लहरों के बीच से अंजलि में उठाए शीतल जल-सा पिघलती, मचलती लहरों में प्रवहमान जल का अपना सच होता है। अंजलि में समाए जल का अपना।
अंजलि का यही जल मेरा सच है। मैं इससे तृप्त हूँ। यह तृप्ति लेखन की नहीं है, जीवन के प्राप्य और प्राप्ति के सामंजस्य की है। मुझे नहीं लगता कि जीवन खोकर लेखन या लेखन छोड़कर ही जीवन को समग्रत: पाया जा सकता है। यथार्थ में दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। जो जीवन में अतल तक नहीं डूबा, उसके लेखन में क्या उतराएगा....और जीवन के ऊपरी तमाशबीनी नहीं, गहरी मार्मिकता चाहिए लेखक को। तब शायद लेखन का विरोध जीवन से नहीं, लेखन कर्म से जुड़ी विरूपताओं और आपाधापियों से है। लेखन अब सुख नहीं, प्रतिस्पर्द्धी महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बन गया है। लोग कहते हैं तो इसमें बुरा क्या है। यह तो हमेशा से हर देश के साहित्य और लेखन के साथ होता आया है। प्रतिस्पर्धा बेहतर लेखन की प्रेरणा बनती है, लेखन में चुनौतियों को स्वीकारने की स्फूर्ति और ऊर्जा भरती है, साहित्य को समद्ध करती है।
लेकिन मुझे तो लगता है, कितना अच्छा हुआ जो कबीर, तुलसी और सूर के समय में ऐसी चुनौतियाँ और प्रेरणाएँ नहीं थीं। मीरा साहित्य-सृजन के इन उपादानों की बेचैनियों से मुक्त थीं। स्पर्द्धा और होड़ा-होड़ी रीतिकालीन स्थितियों की माँगें थीं, मानसिकता थीं, जिसका प्रभाव समूचे रीति काव्य में दृष्टिगत होता है। वहाँ उपादान बहुत हैं, चाव भी; भाव कम। विश्व के उत्कृष्टम ग्रन्थों की रचना ऐसी प्रेरणाओं से विहीन, उद्दीपनहीन स्थितियों में ही होती रही है। प्राय: प्रतिस्पर्द्धी और तथाकथित चुनौतियों से ठस्समठस्स माहौल में, मात्रा में कहीं ज्यादा, लाउड और सामयिक मुद्दों की धार में भरपूर डुबकी लगानेवाला ट्रेंडी लेखन भले हो जाए, आत्मा में पैठकर उसमें उजास भरनेवाला लेखन अपेक्षाकृत कम हो पाता है। होता भी है तो ऊँची उछाल भरने की असमर्थता की वजह से ऊपर नहीं आ पाता। वर्चस्व, सामाजिक, राजनीतिक विरूपताओं पर उतने ही विरूप प्रहार करनेवाली दबंगई और पूर्वाग्रही निष्कर्षों का ही होता है। दुर्द्धर्ष वैचारिकता तथा प्रतिमा का ऐसा एकांगी इस्तेमाल अकसर देखने को मिल जाता है। वहाँ दृष्टि के विस्तार को बलात् समेटा जा सकता है, पक्षी के पंख काटकर पिंजरे में बंद कर लेने की तरह। अपनी ही प्रतिभा, पारदर्शिता और वैचारिक क्षमता के पंख कतरने की यह प्रवृत्ति काफी कुछ मानव बमों की तरह सर्वग्रामी और आत्मघाती एक साथ होती है।
क्या आज के माहौल में किसी ऐसे रचनाकार की कल्पना की जा सकती है जो अपने आपको चारों तरफ से घोर व्यावयायिक दबावों से मुक्त रखकर लेखन कर सके ? व्यावसायिकता से मेरा आशय समाज में नहीं, लेखन के क्षेत्र में व्याप्त निरंकुश व्यावसायिक स्थितियों से है। हर लेखक के चेतन अवचेतन में कमोबेश इन व्यापारों का व्यामोह पलता ही है। पुरस्कारों, अनुदानों, पुस्तक मेलों और लोकार्पणों, उद्घाटनों को लेकर जो हास्यास्पद दौड़े लगती हैं, समय और शक्ति का जो अपव्यय होता है, जो हडबोंग मचती है उसे देखकर यही लगता है कि आज सफल लेखक के लिए सफल व्यवसायी होना ज्यादा जरूरी है। अब बाजार की माँग की पूर्ति तो होनी ही है, इसलिए देखते-देखते एक लेखक की शख्सियत का बहुतांश व्यवसायी होता चला जाता है। यहाँ तक कि बाकी रोजगारियों के तो कुछ असूल होते भी हों, लेकिन यह त्वरित उपलब्धि का उतावला व्यवसायी इस ‘धंधे’ में सबकुछ ‘जायज’ कर चलने का अभ्यस्त हो जाता है।
लोग चाहे तो कहें, लेकिन मुझे लगता है, लेखक सिर्फ उतना भर ही नहीं है जितना वह कागज पर उतारता है, वह उससे बहुत ज्यादा है। कागज पर उतरने-उतराने के बाद बचे इस लेखक-शेष का भी, नीति की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, वृत्ति, प्रवृत्ति और संवेदना से उतना ही समृद्ध भरपूर होना है जितना वह कागजों पर उतारता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अपनी सारी संवेदना कागजों पर ही खर्च कर मुक्त हो जाए और एक मामूली इन्सान भर भी इनसान न रह जाए। क्या लेखन से बड़ी महत्त्वाकांक्षा अपने अंदर के इनसान को बचाए रखने की नहीं चाहिए ? कागज पर उतरने और जीवन में विचरनेवाले लेखक के बीच उभयनिष्ठ रंग-रेखाएँ नहीं होंगी तो पढ़नेवाले अपना विश्वास कहाँ रोपेंगे ? वे अपने लिए आधार और आलंबन कहाँ ढूढ़ेंगे ? मुझे मालूम है, यह देश-विदेश के सैकड़ों ऐसे कलाकारों, साहित्यकारों के जीवन और लेखन के बीच की परस्पर प्रतिरोधी मिसालें दी जा सकती हैं। यह भी कि बावजूद इन विपरीत गुणों के उनकी कृतियाँ अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कीर्तिमान बना चुकी हैं, किन कीर्तिमानों का गणित हमेशा जीवन का कुतुबनुमा नहीं हुआ करता। मात्र अति बौद्धिकता में ही अथ और इति को प्राप्त होनेवाली कृतियों से जीवन-दिशाएँ नहीं बदला करतीं। उन्हें असल और निष्पक्ष चाहिए होता है और ये ही दोनों बुरी तरह उलझते-पुलझते गए हैं इस पूरी शताब्दी में। उलझाव का संक्रमण कर समर्थ रहा है यह....और सुलझानेवाली शक्तियाँ लगातार क्षरित होती रही हैं। अन्यथा सारी इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजिकल मारामारी के बावजूद आदमी आज ज्यादा सहूलियत से जिंदा रह पाता। संवेदना की जो विरासतें कला और साहित्य के माध्यम से उसे मिल सकती थीं, नहीं मिल पाईं।
इसलिए अपने अपराध-बोध को बहुत गैर जरूरी नहीं मान पाती मैं; क्योंकि है तो यह भी किसी संवेदना के घनत्व के बीच से ही उपजा। तो पहली आश्वस्ति तो यही कि कम-से-कम, संवेदना की यह संजीवनी, जिलाए रखेगी मेरे अंदर के लेखक और आदमी को भी। मुझे सोचने पर विवश भी करती रहेगी कि अपने जीवन और लेखन की विभाजित भूमिकाओं में मैं कितनी खरी उतर पा रही हूँ, कितनी ईमानदारी बरत रही हूँ ? अपने ‘देय’ के प्रति कितनी सजग और सचेष्ट हूँ ? दुकान छोटी ही सही, माल में मिलावटी घालमेल तो नहीं ? एक बात और, माल कितना भी
भरा हो, लेकिन बेचना वह है जिसकी लोगों को आज जरूरत है।
‘पाँच लंबी कहानियाँ’ इस जरूरत को थोड़ा-बहुत पूरा करती हैं, इस संतोष के साथ –
-सूर्यबाला
गृह प्रवेश
बीरू की चिट्टी आई है। गृह प्रवेश पर बुलाया है। खूब गुस्से से, खूब प्यार
से, खूब ताने-तिश्ने और उलहाने से, बचपन की एक हजार एक कसमों का हवाला
देकर और बाद में यह जोड़कर कि ‘कुन्नी-मुन्नी’ (मेरी
बेटियाँ)
मामा को न पहचानें और राजा, बंटू के चेहरे पर बुआ का नाम लेने पर एक
हैरत-सी पड़ जाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात भला और क्या हो सकती है। तो
अपनी खातिर, मेरी भी खातिर न सही, इन बच्चों की खातिर कि बुआ इनके लिए एक
कहानी बनकर न रह जाए। तो देखता हूँ, दिन-मुहूर्त और इत्तिला करता हूँ
पंद्रह दिन पहले, जिससे जीजाजी फिर से ‘छुट्टी नहीं
मिली’
वाला वह बासा-उबासा बहाना न दुहराएँ। सचमुच विश्वास नहीं होता कि
तुम....तुम वही दीदी हो जो....जाने दो...’
मैं लपकर जैसे बीरू का हाथ पकड़कर कह उठती हूँ – ‘जाने क्यों दो ? रुक क्यों गया ? बोल न कि वही दीदी हो जो....जो तुझे पीठ पर घुड़ैया लादकर यहाँ से वहाँ दौड़ती फिरती थी। जो रजाइयों के ढेर पर तुझे गेंद की तरह उछाल-उछालकर खिलखिलाती थी और कभी कभी बात न मानने पर तेरे कान ऐंठकर धमाधम घूँसे जड़ दिया करती थी, क्योंकि तूने उसकी चुन्नी धूल में लथोरी होती थी। उसकी सुलेख की कॉपी पर दवात ढुलकाई होती थी (अनजाने नहीं, जान-बूझकर, दुष्टताई से)। उसकी चोटी के रिबन से उसे ही घोड़ी बनाकर टिकटिकाया होता और खेल के बीच दौड़कर उसकी फ्रॉक से नाक पोंछ ली होती।
तो तू बड़ा नालायक था, तू बेहद शरारती था, बला का हुड़दंगी; लेकिन मेरा सबसे प्यारा दोस्त !
मैं लाड़ और ममता से रुँधी-रुँधी गीली हथेलियों में चिट्ठी दबाए सारे घर में डोलती फिरी। दोनों बच्चियों को तोरई छीलते, कपड़े तहाते, ‘बीरू मामा’ और ‘शकुन मामी’ और राजा, बंटू की बातें बताती रही –
‘‘मामा छोटा था तो लंबे पुछल्ले लगाकर रंग-बिरंगी पतंगें उड़ाता था। मुँडेरों नीचे छिप-छिपकर पेंग मारती पतंगों को धागों में कंकड़ बाँधकर काटता था और फटाक् उन्हें बरसाती में रखी बोरी के नीचे छिपा आता था। लड़कों के साथ ‘ऊँचे पर का गाजगू’ और लड़कियों के साथ ‘चाक-चाक चालन’ खेलता था और सबके सामने एक-दूसरे का स्वाँग उतारकर हँसा-हँसाकर लहालोट करता रहता था। वह किसी भी मेले, तमाशे, शादी-ब्याह, नाते-रिश्ते में जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। जो दो-चार जोड़ी कमीजें-निकरें ही साफ-सूफ कर, लोहा मार, फिट्ट-तैयार...बचपन से ही, जहाँ जाता वहीं खूब खेल-खा हुड़दंग-तमाशे कर खुश-खुश वापस लौटता। माँ से चाँटे खाने या पिटने के बाद भी एकाध आँसू दर्द के मारे भले ही निकल जाए, बाकी को सँभालता, उलटे उन्हें ही चिढ़ाता भाग निकलता।
‘‘बहुत छुटपन में सिर्फ एक बार उसे थोड़ा उदास देखा था। जब पड़ोस की एक लड़की शादी के बाद विदा हो रही थी और सबसे लिपट-लिपटकर धार-धार रो रही थी। अपने बरामदे से देखते-देखते उसने मुझसे पूछा था, ‘दीदी ! तेरी शादी हो जाएगी तो तू भी चली जाएगी क्या ?’
‘और नहीं तो क्या मैं जिंदगी भर यहीं बैठी रहूँगी ?’ मैंने निखालिस बड़ी-बूढ़ियों-सा सयानापन ओढ़ते हुए कहा था; लेकिन तत्क्षण शायद भाई की और खुद अपने अंदर घिरती उदासी से निजात पाने के लिए सयानी लड़कियों की-सी बतकचरेवाली खास अदा से कहा, ‘लेकिन तू फिकर मत कर, मैं ‘तेरे जीजाजी’ को समझा-बुझाकर तेरे पास आ जाया करूँगी।’
‘‘ ‘हाँ-हाँ, तब हम फिर से ‘चाक-चाक चालन’ खेलेंगे।’ भाई खुश हो गया था।
‘‘ ‘भक्क ! तब तक तो मैं मम्मी बन जाऊँगी। कहीं मम्मी बनने के बाद कोई चाक-चाक...’
‘‘कि, ‘चाट्ट’ से पीछे से आई माँ का भरपूर चाँटा मेरे गाल पर पड़ा।
‘‘ ‘बेशर्म ! बेहया ! बित्ते भर की छोकरी का दीदा देखो। पढ़ाई-लिखाई तो दरकिनार, ‘जीजाजी’ के हौसले बाँध रही है। दोनों को डपटकर पढ़ाई करने के लिए बिठाया था न ?... वह सब छोड़-छाड़कर यहाँ आकर गलचौरा कर रही है। और तो और, लाज-शर्म घोल-घाल मम्मी बनने की मातबरी बखान रही है...बेशर्म कहीं की !’ ’’
उस समय माँ के तमतमाने का साफ-साफ कोई भी कारण समझ में नहीं आया था, पर छोटे भाई के सामने माँ से चाँटा खाने की वजह से मैं एकदम अपमानित-सी खड़ी रह गई थी। तभी भाई को जाने क्या सूझा, उसने माँ को जोर से मुँह चिढ़ाया और भाग खड़ा हुआ। माँ लपककर उसे पकड़ने की कोशिश करती रही और वह वहीं बरामदे में बिछी खाट के चारों ओर बच-बचाकर भागता रहा, जैसे माँ के साथ पकड़म-पकड़ाई खेल रहा हो। और वह तब तक भागता रहा जब तक खाट के चारों ओर लस्त-पस्त दौड़ती माँ और भाई के हुलिए पर, गालों पर ढुलकी आँसुओं की धार के बीच मैं खुद खिलखिलाकर हँस न पड़ी।
‘जाने’ के नाम पर बच्चियाँ चकेरी मार-मारकर उछलने लगीं – मामा के घर जाएँगे, दूध-मलाई खाएँगे, आइसक्रीम खाएँगे। आइसक्रीम महँगी होती है तो ठीक है। छोटी वाली टॉफी खाएँगे।...और अटरम-शटरम जो पातीं, मेरे बक्से में ला-लाकर डाल जातीं। यह टोपा मामा के छोटेवाले भैया, क्या नाम है उसका – राजा को आएगा न...और यह कंजी आँखोंवाली गुड़िया मीनू को देंगे। सिर्फ इसके बाल ही तो उलझे-पुलझे हैं तो हम साबुन- रीठे से धोए लेते हैं।
‘‘मामा के शहर में चिड़ियाघर है क्या, मम्मी ? और चिल्ड्रेन पार्क ? उसमें अगर हाथी भी बना हो तो हम उसकी सूड़ में से घुसकर दुम के नीचे से निकल आएँ।’’
‘‘छिह ! गंदी ! खी-खी-खी-खी !’’ बड़ीवाली छोटीवाली पर खिलखिला पड़ी।
मैंने भी खूब-खूब कपड़े धोए, कलफ डाली, उधड़ी सीवनों की मरम्मत की। घर और बाहर पहनने के कपड़े अलगाए और कटपीस के टुकड़े ला-लाकर भाई के बच्चों के लिए कपड़े सिले।
लेकिन जाने की शाम ये हड़बड़ाए हुए लौटे ऑफिस से और घर के सारे दरवाजे अंधाधुंध अंदर से बंद करते हुए हाँफती आवाज में बोले, ‘‘जाना नहीं हो सकता। पूरे चौक ऐरिया में जबरदस्त सनसनी है। दुकानों के शटर खटाखट बंद हो रहे हैं। नई सड़क तक जिसे देखो, दुकान डलिया समेटे जल्दी-जल्दी घर भागने की फिराक में रिक्शा-ऑटो तलाश रहा था – अजब बदहवासी का आलम – बाजार, सड़क देखते-देखते वीरान। गश्ती पुलिस के सिपाही बेरहमी से डंडे ठकठकाते घूम रहे हैं।’’
‘‘लेकिन...लेकिन हुआ क्या ?’’ घबराहट से ज्यादा हैरत तारी थी मुझपर।
‘‘हुआ जो कुछ भी हो, लेकिन उससे कही ज्यादा होने का अंदेशा है।’’
आवाज की बदहवाली कायम थी।
‘‘फिर भी आखिर कुछ तो हुआ होगा।’’
‘‘क्या वाहियात बात करती हो ? जैसे तुम जानतीं नहीं, क्या होता है ऐसे मौकों पर ? क्या होता आया है पिछली मर्तबा और उससे भी पहले हर बार – उससे अलग या उससे भी ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है ?’’
मैंने उस खौफ और गुस्से को नरमी से सहलाते हुए कहा, ‘‘नहीं, असल में इस सिरे पर ऐसी कुछ ज्यादा दहशत या सन्नाटा नहीं है न – इसलिए पूछ रही थी कि सचमुच कुछ ज्यादा गड़बड़ है या सिर्फ अंदेशे की बदहवासी... ’’
‘‘सिर्फ अंदेशे की बदहवासी ? लोग क्या पागल हैं ? उन्हें क्या पता नहीं कि अंदेशों को सच होते कितनी देर लगती है। वे सैकड़ों बार ऐसी स्थितियों का हश्र भुगत चुके हैं, इसलिए अगर ऐसी भनक लगते ही थरथर काँपते, जान की दुआ माँगते बदहवासी में भागते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं ?’’
‘‘गलत की बात कहाँ ? लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कुछ और न हो या जो कुछ हुआ भी वह जहाँ-का-तहाँ सँभल जाए।’’
‘‘तुम आसानी से घर में बैठी हो न, इसलिए सारी चीजों की सिर्फ कल्पना कर उन्हें अपनी इच्छा-भावना के हिसाब से अगर-मगर करके उलटती रह सकती हो; लेकिन तुम अगर बदहवास लोगों की भीड़ के बीच से भागकर आई होतीं न, तो तुम्हें पता चलता कि छटपटाकर मरने से कहीं ज्यादा त्रासद छटपटाकर मरने का अंदेशा होता है।’’
सचमुच मैं सारी स्थितियों को खींच-खाँचकर सिर्फ एक ही मनसूबे की ओर ला रही थी –
‘‘तब हमारा जाना...?’’ मेरी आवाज तेजी से जैसे गहरे जल में डूबती जा रही थी।
‘‘दिमाग तो सही है तुम्हारा ? शहर में किसी भी क्षण उबाल आना चाहता है और तुम स्टेशन जाने के मनसूबे बाँध रही हो ! होश-हवास दुरुस्त हों तो जरा मेरी हालत पर रहम कर एक कप चाय बना दो। उफ !’’
बच्चियाँ कोने में सहमी हमारी बातें सुन रही थीं। मैंने उनसे कहा, ‘‘हम नहीं जा पाएँगे।’’ और रास्ते के लिए रच-रचाकर बनाए पुए-पूरियों के कटोरदान उनके आगे खोल दिए। सबके मुँह में फीके स्वाद के डेले पिघलने लगे।
कल भाई स्टेशन आएगा – एक हजार एक कसमों का वास्ता देकर लिखे खत के एवज में हर डिब्बे में फिर झाँक-झाँककर ढूँढ़ेगा। सारा प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा तब भी शायद उसे विश्वास न आए। सोचेगा, दीदी ने इस बार भी दगा दी। और इधर भी तो....टिकट, रिजर्वेशन, छुट्टी। कितनी आरजू-मिन्नतों से जुट पाया था सबकुछ !
बच्चियाँ उदास हो आईं, ‘‘कित्ता गंदा शहर है न, मम्मी ! कित्ते गंदे लोग ! क्यों करते हैं लोग इत्ता झगड़ा यहाँ ? मम्मी, मामा का शहर ऐसा नहीं है न ? अब कब चलेंगे मामा के शहर में ?’’
मैं लपकर जैसे बीरू का हाथ पकड़कर कह उठती हूँ – ‘जाने क्यों दो ? रुक क्यों गया ? बोल न कि वही दीदी हो जो....जो तुझे पीठ पर घुड़ैया लादकर यहाँ से वहाँ दौड़ती फिरती थी। जो रजाइयों के ढेर पर तुझे गेंद की तरह उछाल-उछालकर खिलखिलाती थी और कभी कभी बात न मानने पर तेरे कान ऐंठकर धमाधम घूँसे जड़ दिया करती थी, क्योंकि तूने उसकी चुन्नी धूल में लथोरी होती थी। उसकी सुलेख की कॉपी पर दवात ढुलकाई होती थी (अनजाने नहीं, जान-बूझकर, दुष्टताई से)। उसकी चोटी के रिबन से उसे ही घोड़ी बनाकर टिकटिकाया होता और खेल के बीच दौड़कर उसकी फ्रॉक से नाक पोंछ ली होती।
तो तू बड़ा नालायक था, तू बेहद शरारती था, बला का हुड़दंगी; लेकिन मेरा सबसे प्यारा दोस्त !
मैं लाड़ और ममता से रुँधी-रुँधी गीली हथेलियों में चिट्ठी दबाए सारे घर में डोलती फिरी। दोनों बच्चियों को तोरई छीलते, कपड़े तहाते, ‘बीरू मामा’ और ‘शकुन मामी’ और राजा, बंटू की बातें बताती रही –
‘‘मामा छोटा था तो लंबे पुछल्ले लगाकर रंग-बिरंगी पतंगें उड़ाता था। मुँडेरों नीचे छिप-छिपकर पेंग मारती पतंगों को धागों में कंकड़ बाँधकर काटता था और फटाक् उन्हें बरसाती में रखी बोरी के नीचे छिपा आता था। लड़कों के साथ ‘ऊँचे पर का गाजगू’ और लड़कियों के साथ ‘चाक-चाक चालन’ खेलता था और सबके सामने एक-दूसरे का स्वाँग उतारकर हँसा-हँसाकर लहालोट करता रहता था। वह किसी भी मेले, तमाशे, शादी-ब्याह, नाते-रिश्ते में जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। जो दो-चार जोड़ी कमीजें-निकरें ही साफ-सूफ कर, लोहा मार, फिट्ट-तैयार...बचपन से ही, जहाँ जाता वहीं खूब खेल-खा हुड़दंग-तमाशे कर खुश-खुश वापस लौटता। माँ से चाँटे खाने या पिटने के बाद भी एकाध आँसू दर्द के मारे भले ही निकल जाए, बाकी को सँभालता, उलटे उन्हें ही चिढ़ाता भाग निकलता।
‘‘बहुत छुटपन में सिर्फ एक बार उसे थोड़ा उदास देखा था। जब पड़ोस की एक लड़की शादी के बाद विदा हो रही थी और सबसे लिपट-लिपटकर धार-धार रो रही थी। अपने बरामदे से देखते-देखते उसने मुझसे पूछा था, ‘दीदी ! तेरी शादी हो जाएगी तो तू भी चली जाएगी क्या ?’
‘और नहीं तो क्या मैं जिंदगी भर यहीं बैठी रहूँगी ?’ मैंने निखालिस बड़ी-बूढ़ियों-सा सयानापन ओढ़ते हुए कहा था; लेकिन तत्क्षण शायद भाई की और खुद अपने अंदर घिरती उदासी से निजात पाने के लिए सयानी लड़कियों की-सी बतकचरेवाली खास अदा से कहा, ‘लेकिन तू फिकर मत कर, मैं ‘तेरे जीजाजी’ को समझा-बुझाकर तेरे पास आ जाया करूँगी।’
‘‘ ‘हाँ-हाँ, तब हम फिर से ‘चाक-चाक चालन’ खेलेंगे।’ भाई खुश हो गया था।
‘‘ ‘भक्क ! तब तक तो मैं मम्मी बन जाऊँगी। कहीं मम्मी बनने के बाद कोई चाक-चाक...’
‘‘कि, ‘चाट्ट’ से पीछे से आई माँ का भरपूर चाँटा मेरे गाल पर पड़ा।
‘‘ ‘बेशर्म ! बेहया ! बित्ते भर की छोकरी का दीदा देखो। पढ़ाई-लिखाई तो दरकिनार, ‘जीजाजी’ के हौसले बाँध रही है। दोनों को डपटकर पढ़ाई करने के लिए बिठाया था न ?... वह सब छोड़-छाड़कर यहाँ आकर गलचौरा कर रही है। और तो और, लाज-शर्म घोल-घाल मम्मी बनने की मातबरी बखान रही है...बेशर्म कहीं की !’ ’’
उस समय माँ के तमतमाने का साफ-साफ कोई भी कारण समझ में नहीं आया था, पर छोटे भाई के सामने माँ से चाँटा खाने की वजह से मैं एकदम अपमानित-सी खड़ी रह गई थी। तभी भाई को जाने क्या सूझा, उसने माँ को जोर से मुँह चिढ़ाया और भाग खड़ा हुआ। माँ लपककर उसे पकड़ने की कोशिश करती रही और वह वहीं बरामदे में बिछी खाट के चारों ओर बच-बचाकर भागता रहा, जैसे माँ के साथ पकड़म-पकड़ाई खेल रहा हो। और वह तब तक भागता रहा जब तक खाट के चारों ओर लस्त-पस्त दौड़ती माँ और भाई के हुलिए पर, गालों पर ढुलकी आँसुओं की धार के बीच मैं खुद खिलखिलाकर हँस न पड़ी।
‘जाने’ के नाम पर बच्चियाँ चकेरी मार-मारकर उछलने लगीं – मामा के घर जाएँगे, दूध-मलाई खाएँगे, आइसक्रीम खाएँगे। आइसक्रीम महँगी होती है तो ठीक है। छोटी वाली टॉफी खाएँगे।...और अटरम-शटरम जो पातीं, मेरे बक्से में ला-लाकर डाल जातीं। यह टोपा मामा के छोटेवाले भैया, क्या नाम है उसका – राजा को आएगा न...और यह कंजी आँखोंवाली गुड़िया मीनू को देंगे। सिर्फ इसके बाल ही तो उलझे-पुलझे हैं तो हम साबुन- रीठे से धोए लेते हैं।
‘‘मामा के शहर में चिड़ियाघर है क्या, मम्मी ? और चिल्ड्रेन पार्क ? उसमें अगर हाथी भी बना हो तो हम उसकी सूड़ में से घुसकर दुम के नीचे से निकल आएँ।’’
‘‘छिह ! गंदी ! खी-खी-खी-खी !’’ बड़ीवाली छोटीवाली पर खिलखिला पड़ी।
मैंने भी खूब-खूब कपड़े धोए, कलफ डाली, उधड़ी सीवनों की मरम्मत की। घर और बाहर पहनने के कपड़े अलगाए और कटपीस के टुकड़े ला-लाकर भाई के बच्चों के लिए कपड़े सिले।
लेकिन जाने की शाम ये हड़बड़ाए हुए लौटे ऑफिस से और घर के सारे दरवाजे अंधाधुंध अंदर से बंद करते हुए हाँफती आवाज में बोले, ‘‘जाना नहीं हो सकता। पूरे चौक ऐरिया में जबरदस्त सनसनी है। दुकानों के शटर खटाखट बंद हो रहे हैं। नई सड़क तक जिसे देखो, दुकान डलिया समेटे जल्दी-जल्दी घर भागने की फिराक में रिक्शा-ऑटो तलाश रहा था – अजब बदहवासी का आलम – बाजार, सड़क देखते-देखते वीरान। गश्ती पुलिस के सिपाही बेरहमी से डंडे ठकठकाते घूम रहे हैं।’’
‘‘लेकिन...लेकिन हुआ क्या ?’’ घबराहट से ज्यादा हैरत तारी थी मुझपर।
‘‘हुआ जो कुछ भी हो, लेकिन उससे कही ज्यादा होने का अंदेशा है।’’
आवाज की बदहवाली कायम थी।
‘‘फिर भी आखिर कुछ तो हुआ होगा।’’
‘‘क्या वाहियात बात करती हो ? जैसे तुम जानतीं नहीं, क्या होता है ऐसे मौकों पर ? क्या होता आया है पिछली मर्तबा और उससे भी पहले हर बार – उससे अलग या उससे भी ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है ?’’
मैंने उस खौफ और गुस्से को नरमी से सहलाते हुए कहा, ‘‘नहीं, असल में इस सिरे पर ऐसी कुछ ज्यादा दहशत या सन्नाटा नहीं है न – इसलिए पूछ रही थी कि सचमुच कुछ ज्यादा गड़बड़ है या सिर्फ अंदेशे की बदहवासी... ’’
‘‘सिर्फ अंदेशे की बदहवासी ? लोग क्या पागल हैं ? उन्हें क्या पता नहीं कि अंदेशों को सच होते कितनी देर लगती है। वे सैकड़ों बार ऐसी स्थितियों का हश्र भुगत चुके हैं, इसलिए अगर ऐसी भनक लगते ही थरथर काँपते, जान की दुआ माँगते बदहवासी में भागते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं ?’’
‘‘गलत की बात कहाँ ? लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कुछ और न हो या जो कुछ हुआ भी वह जहाँ-का-तहाँ सँभल जाए।’’
‘‘तुम आसानी से घर में बैठी हो न, इसलिए सारी चीजों की सिर्फ कल्पना कर उन्हें अपनी इच्छा-भावना के हिसाब से अगर-मगर करके उलटती रह सकती हो; लेकिन तुम अगर बदहवास लोगों की भीड़ के बीच से भागकर आई होतीं न, तो तुम्हें पता चलता कि छटपटाकर मरने से कहीं ज्यादा त्रासद छटपटाकर मरने का अंदेशा होता है।’’
सचमुच मैं सारी स्थितियों को खींच-खाँचकर सिर्फ एक ही मनसूबे की ओर ला रही थी –
‘‘तब हमारा जाना...?’’ मेरी आवाज तेजी से जैसे गहरे जल में डूबती जा रही थी।
‘‘दिमाग तो सही है तुम्हारा ? शहर में किसी भी क्षण उबाल आना चाहता है और तुम स्टेशन जाने के मनसूबे बाँध रही हो ! होश-हवास दुरुस्त हों तो जरा मेरी हालत पर रहम कर एक कप चाय बना दो। उफ !’’
बच्चियाँ कोने में सहमी हमारी बातें सुन रही थीं। मैंने उनसे कहा, ‘‘हम नहीं जा पाएँगे।’’ और रास्ते के लिए रच-रचाकर बनाए पुए-पूरियों के कटोरदान उनके आगे खोल दिए। सबके मुँह में फीके स्वाद के डेले पिघलने लगे।
कल भाई स्टेशन आएगा – एक हजार एक कसमों का वास्ता देकर लिखे खत के एवज में हर डिब्बे में फिर झाँक-झाँककर ढूँढ़ेगा। सारा प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा तब भी शायद उसे विश्वास न आए। सोचेगा, दीदी ने इस बार भी दगा दी। और इधर भी तो....टिकट, रिजर्वेशन, छुट्टी। कितनी आरजू-मिन्नतों से जुट पाया था सबकुछ !
बच्चियाँ उदास हो आईं, ‘‘कित्ता गंदा शहर है न, मम्मी ! कित्ते गंदे लोग ! क्यों करते हैं लोग इत्ता झगड़ा यहाँ ? मम्मी, मामा का शहर ऐसा नहीं है न ? अब कब चलेंगे मामा के शहर में ?’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i