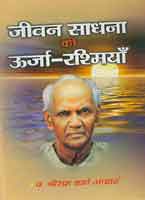|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोगश्रीराम शर्मा आचार्य
|
111 पाठक हैं |
||||||
आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग
सर्वशक्तिमान् परमेश्वर और उसका सान्निध्य
सर्वशक्तिमान् परमेश्वर और उसका सान्निध्य
प्रत्येक कर्म का कोई अधिष्ठाता जरूर होता है। परिवार के वयोवृद्ध मुखिया
के हाथ सारी गृहस्थी का नियन्त्रण होता है, मिलों -कारखानों की देखरेख के
लिए मैनेजर होते हैं, राज्यपाल-प्रान्त के शासन की बागडोर सँभालते हैं,
राष्ट्रपति सम्पूर्ण राष्ट्र का स्वामी होता है। जिसके हाथ में जैसी
विधि-व्यवस्था होती है उसी के अनुरूप उसे अधिकार भी मिले होते हैं।
अपराधियों को दण्ड व्यवस्था, सम्पूर्ण प्रजा के पालन-पोषण और न्याय के
लिये उन्हें उसी अनुपात से वैधानिक या सैद्धान्तिक अधिकार प्राप्त होते
हैं। अधिकार न दिये जायें तो लोग स्वेच्छाचारिता, छल-कपट और निर्दयता का
व्यवहार करने लगें। न्याय व्यवस्था के लिये शक्ति और सत्तावान होना उपयोगी
ही नहीं आवश्यक भी है।
इतना बड़ा संसार एक निश्चित व्यवस्था पर ठीक-ठिकाने चल रहा है, सूरज प्रतिदिन ठीक समय से निकल आता है, चन्द्रमा की क्या औकात जो अपनी माहवारी ड्यूटी में रत्ती भर फर्क डाल दे, ऋतुएँ अपना समय आते ही आती और लौट जाती हैं, आम का बौर बसन्त में ही आता है, टेसू गर्मी में ही फूलते हैं, वर्षा तभी होती है जब समुद्र से मानसून बनता है। सारी प्रकृति, सम्पूर्ण संसार ठीक व्यवस्था से चल रहा है, जो जरा सा इधर उधर हुए कि उसने मार खाई। अपनी कक्षा से जरा डाँवाडोल हुए कि एक तारे को दूसरा खा गया। जीवन-क्रम में थोड़ी भूल हुई कि रोग-शोक, बीमारी और अकाल-मृत्यु ने झपट्टा मारा। इतने बड़े संसार का नियामक परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली है। सत्तावान न होता हो कौन उसकी बात सुनता। दण्ड देने में उसने चूक की होती तो अनियमितता, अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था ही रही होती। उसकी सृष्टि से कोई भी छुपकर पाप और अत्याचार नहीं कर सकता। बड़ा कठोर है वह, दुष्ट को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिये वेद ने आग्रह किया है—
इतना बड़ा संसार एक निश्चित व्यवस्था पर ठीक-ठिकाने चल रहा है, सूरज प्रतिदिन ठीक समय से निकल आता है, चन्द्रमा की क्या औकात जो अपनी माहवारी ड्यूटी में रत्ती भर फर्क डाल दे, ऋतुएँ अपना समय आते ही आती और लौट जाती हैं, आम का बौर बसन्त में ही आता है, टेसू गर्मी में ही फूलते हैं, वर्षा तभी होती है जब समुद्र से मानसून बनता है। सारी प्रकृति, सम्पूर्ण संसार ठीक व्यवस्था से चल रहा है, जो जरा सा इधर उधर हुए कि उसने मार खाई। अपनी कक्षा से जरा डाँवाडोल हुए कि एक तारे को दूसरा खा गया। जीवन-क्रम में थोड़ी भूल हुई कि रोग-शोक, बीमारी और अकाल-मृत्यु ने झपट्टा मारा। इतने बड़े संसार का नियामक परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली है। सत्तावान न होता हो कौन उसकी बात सुनता। दण्ड देने में उसने चूक की होती तो अनियमितता, अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था ही रही होती। उसकी सृष्टि से कोई भी छुपकर पाप और अत्याचार नहीं कर सकता। बड़ा कठोर है वह, दुष्ट को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिये वेद ने आग्रह किया है—
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः।
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मैदेवाय हविषा विधेम।।
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मैदेवाय हविषा विधेम।।
ऋ. वेद 10।121।4
हे मनुष्यों ! बर्फ से आच्छादित पहाड़, नदियाँ, समुद्र जिसकी महिमा का
गुणगान करते हैं। दिशायें जिसकी भुजायें हैं हम उस विराट् विश्व पुरुष
परमात्मा को कभी न भूलें।
गीता के ‘‘येन सर्वविदं ततम्’’ अर्थात् ‘‘यह जो कुछ है परमात्मा से व्याप्त है’’ की विशद व्याख्या करते हुये योगीराज अरविन्द ने लिखा है—
‘‘यह सम्पूर्ण संसार परमात्मा की ही सावरण अभिव्यंजना है। जीव की पूर्णता या मुक्ति और कुछ नहीं भगवान् के साथ चेतना, ज्ञान, इच्छा, प्रेम और आध्यात्मिक सुख में एकता प्राप्त करना तथा भगवती शक्ति के कार्य सम्पादन में अज्ञान, पाप आदि से मुक्त होकर सहयोग देना है। यह स्थिति उसे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक आत्मा अहंकार के पिंजरे में कैद है, अज्ञान में आवृत है तथा उसे आध्यात्मिक शक्तियों की सत्यता पर विश्वास नहीं होता। अहंकार का जाल, मन, शरीर, जीवन, भाव, इच्छा, विचार, सुख और दुःख के संघर्ष, पाप, पुण्य, अपना पराया आदि के जटिल प्रपंच मनुष्य में स्थित एक उच्चतर आध्यात्मिक शक्ति के ब्रह्म और अपूर्ण रूपमात्र हैं। महत्ता इसी शक्ति की है, मनुष्य की नहीं, जो प्रच्छन्न रूप से आत्मा में अधिगत है।’’
योगीराज के इस निबन्ध से तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त व्यक्त्त होते हैं। (1) यह जो संसार है परमात्मा से व्याप्त है उसके अतिरिक्त और सब मिथ्या है, भ्रम है, स्वप्न है। (2) मनुष्य को उसकी इच्छानुसार सृष्ठि-संचालन के लिये कार्य करते रहना चाहिये। (3) मनुष्य में जो श्रेष्ठता, शक्ति या, सौन्दर्य है वह उसके दैवी गुणों के विकास पर ही है।
मनुष्य जीवन के सुख और उसकी शान्ति के लिये इन तीनों सिद्धान्त का पालन ऐसा ही पुण्य फलदायक है जैसा त्रिवेणी स्नान करना। मनुष्य दुष्कर्म अहंकार से प्रेरित होकर करता है पर वह बड़ा क्षुद्र प्राणी है, जब परमात्मा की मार उस पर पड़ती है तो बेहाल होकर रोता चिल्लाता है। सुख तो उसकी इच्छाओं के अनुकूल सात्विक दिशा में चलने में, प्राकृतिक नियमों के पालन करने में ही है। अपनी क्षणिक शक्ति के घमण्ड में आया हुआ मनुष्य कभी सही मार्ग पर नहीं चलता इसीलिये उसे सांसारिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। परमात्मा ने यह व्यवस्था इतनी शानदार बनाई है कि यदि सभी मनुष्य इसका पालन करने लगें तो इस संसार में एक भी प्राणी दुःखी और अभावग्रस्त न रहे।
ईश्वर उपासना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। नदियाँ जब तक समुद्र में नहीं मिल जातीं अस्थिर और बेचैन रहती है। मनुष्य की असीमता भी अपने आपको मनुष्य मान लेने की भावना से ढकी हुई है। उपासना विकास की प्रक्रिया है। संकुचित को सीमा रहित करना, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की ओर अग्रसर होना, ‘‘मैं’’ और मेरा छुड़ाकर ‘हम’ और ‘हमारे’ की आदत डालना ही मनुष्य के आत्म-तत्व की ओर विकास की परम्परा है। यही तभी सम्भव है जब सर्वशक्तिमान परमात्मा को स्वीकार कर लें, उसकी शरणागति की प्राप्ति हो जाय। मनुष्य रहते हुए मानवता की सीमा को भेदकर उसे देवस्वरूप में विकसित कर देना ईश्वर की शक्ति का कार्य है। उपासना का अर्थ परमात्मा से उस शक्ति को प्राप्त करना ही है।
जान-बूझकर या अकारण परमात्मा कभी किसी को दण्ड नहीं देता। प्रकृति की स्वच्छन्द प्रगति प्रवृत्ति में ही सबका हित नियन्त्रित है। जो इस प्राकृतिक नियम से टकराता है वह बार-बार दु:ख भोगता है और तब तक चैन नहीं पाता जब तक वापस लौटकर फिर उस सही मार्ग पर नहीं चलने लगता। भगवान् भक्त की भावनाओं का फल तो देते हैं किन्तु उनका विधान सभी संसार के लिये एक जैसा ही है। भावनाशील व्यक्ति भी जब तक अपने पाप की सीमायें नहीं पार कर लेता तब तक अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय रखते हुए भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता।
अपने से विमुख प्राणियों को भी वे दु:ख दण्ड नहीं देता दुख दण्ड देने के लिए शक्ति तो उसके विधान में ही है। मनुष्य का विधान तो देश, काल और परिस्थितियों वश बदलता ही रहता है। किन्तु उसका विधान सदैव एक जैसा ही है। भावनाशील व्यक्ति भी उसकी चाहे कितनी ही उपासना करे सांसारिक कर्त्तव्यों की अवहेलना कर या दैवी-विधाना का उल्लंघन कर कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसा कर्मबीज वैसा ही फल यह उसका निश्चल विधान है। दूसरों का तिरस्कार करने वाला कई गुना तिरस्कार पाता है। परमार्थ उसी तरह लौटकर असंख्य गुने सुख पैदाकर मनुष्य को तृप्त कर देता है। सुख और दु:ख, बन्धन और मुक्ति मनुष्य के कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। दुष्कर्मों का फल भोगने से मनुष्य बच नहीं सकता इस विधान में कहीं राई रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है।
अशुभ कर्मों का सम्पादन और देह का जड़ अभिमान ही मनुष्य को छोटा बनाये हुये है। शुभ-अशुभ कार्यों के फलस्वरूप सुख-दु:ख का भोक्ता न होने पर भी आत्मा मोह वश होकर दु:ख भोगती है। मैं देह हूँ ‘‘मुझे सारे अधिकार मिलने ही चाहिये’’ यह मान लेने से जीव स्वयं कर्त्ता-भोक्ता बन जाता है और इसी कारण वह ‘‘जीव’’ कहलाता है। जब तक वह इतनी -सी सीमा में रहता है तब तक उसकी शक्ति भी उतनी ही तुच्छ और संकुचित बनी ही रहती है। जब वह इस भ्रम रूप देहाध्यास का परित्याग कर देता है तो वह शिव-स्वरूप, ईश्वर-स्वरूप हो जाता है। उसकी शक्तियाँ विस्तीर्ण हो जाती हैं और वह अपने आपकों अनन्त शक्तिशाली, अनन्त आनन्द में लीन हुआ अनुभव करने लगता है।
अपनी तुच्छ सत्ता को परमात्मा की शरणगति में ले जाने से मनुष्य अनेकों कष्ट-कठिनाइयों से बच जाता है। गृहपति की अवज्ञा करके जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सुखी नहीं रह सकता उसी प्रकार परमात्मा का विरोधी भी कभी सुखी या सन्तुष्ट नहीं रह सकता। परमात्मा की अवमानना का अर्थ है उसके सार्वभौमिक नियमों का पालन न करना। अपने स्वार्थ, अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिये कोई भी अनुचित कार्य परमात्मा को प्रिय नहीं। इस तरह की क्षुद्र बुद्धि का व्यक्ति ही उसके कोप का भाजन बनता है पर जो विश्व-कल्याण की कामना में ही अपना कल्याण मानते और तदनुसार आचरण करते हैं। ईश्वर के अनुदान उन्हें उसी तरह प्राप्त होते हैं जैसे कोई पिता अपने सदाचारी, आज्ञा पालक और सेवा भावी पुत्र को ही अपनी सुख-सुविधाओं का अधिकांश भाग सौंपता है।
पापों का नाश हुये बिना, इन्द्रियों का दमन किये बिना, अन्त:करण की शुद्धि नहीं होती। संसार में रहते हुये मनुष्य कर्मों से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। अत: निष्काम कर्मयोग परमात्मा की प्राप्ति और सांसारिक सुखोपभोग का सबसे सुन्दर और समन्वययुक्त धर्म है। निष्काम भावनाओं में पाप नहीं होता वरन दूसरों के हित की, कल्याण की और सबको ऊँचे उठाने की विशालता होती है जिससे अन्त:करण की पवित्रता बढ़ती है और सुख मिलता है अतएव प्रत्येक मनुष्य को संसार समर का योद्धा बनकर ही जीवन यापन करना चाहिए। वह साहस वह गम्भीरता और वह कार्य करने की भावना मनुष्य ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म सान्निध्यता में ही प्राप्त करता है।
गीता के ‘‘येन सर्वविदं ततम्’’ अर्थात् ‘‘यह जो कुछ है परमात्मा से व्याप्त है’’ की विशद व्याख्या करते हुये योगीराज अरविन्द ने लिखा है—
‘‘यह सम्पूर्ण संसार परमात्मा की ही सावरण अभिव्यंजना है। जीव की पूर्णता या मुक्ति और कुछ नहीं भगवान् के साथ चेतना, ज्ञान, इच्छा, प्रेम और आध्यात्मिक सुख में एकता प्राप्त करना तथा भगवती शक्ति के कार्य सम्पादन में अज्ञान, पाप आदि से मुक्त होकर सहयोग देना है। यह स्थिति उसे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक आत्मा अहंकार के पिंजरे में कैद है, अज्ञान में आवृत है तथा उसे आध्यात्मिक शक्तियों की सत्यता पर विश्वास नहीं होता। अहंकार का जाल, मन, शरीर, जीवन, भाव, इच्छा, विचार, सुख और दुःख के संघर्ष, पाप, पुण्य, अपना पराया आदि के जटिल प्रपंच मनुष्य में स्थित एक उच्चतर आध्यात्मिक शक्ति के ब्रह्म और अपूर्ण रूपमात्र हैं। महत्ता इसी शक्ति की है, मनुष्य की नहीं, जो प्रच्छन्न रूप से आत्मा में अधिगत है।’’
योगीराज के इस निबन्ध से तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त व्यक्त्त होते हैं। (1) यह जो संसार है परमात्मा से व्याप्त है उसके अतिरिक्त और सब मिथ्या है, भ्रम है, स्वप्न है। (2) मनुष्य को उसकी इच्छानुसार सृष्ठि-संचालन के लिये कार्य करते रहना चाहिये। (3) मनुष्य में जो श्रेष्ठता, शक्ति या, सौन्दर्य है वह उसके दैवी गुणों के विकास पर ही है।
मनुष्य जीवन के सुख और उसकी शान्ति के लिये इन तीनों सिद्धान्त का पालन ऐसा ही पुण्य फलदायक है जैसा त्रिवेणी स्नान करना। मनुष्य दुष्कर्म अहंकार से प्रेरित होकर करता है पर वह बड़ा क्षुद्र प्राणी है, जब परमात्मा की मार उस पर पड़ती है तो बेहाल होकर रोता चिल्लाता है। सुख तो उसकी इच्छाओं के अनुकूल सात्विक दिशा में चलने में, प्राकृतिक नियमों के पालन करने में ही है। अपनी क्षणिक शक्ति के घमण्ड में आया हुआ मनुष्य कभी सही मार्ग पर नहीं चलता इसीलिये उसे सांसारिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। परमात्मा ने यह व्यवस्था इतनी शानदार बनाई है कि यदि सभी मनुष्य इसका पालन करने लगें तो इस संसार में एक भी प्राणी दुःखी और अभावग्रस्त न रहे।
ईश्वर उपासना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। नदियाँ जब तक समुद्र में नहीं मिल जातीं अस्थिर और बेचैन रहती है। मनुष्य की असीमता भी अपने आपको मनुष्य मान लेने की भावना से ढकी हुई है। उपासना विकास की प्रक्रिया है। संकुचित को सीमा रहित करना, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की ओर अग्रसर होना, ‘‘मैं’’ और मेरा छुड़ाकर ‘हम’ और ‘हमारे’ की आदत डालना ही मनुष्य के आत्म-तत्व की ओर विकास की परम्परा है। यही तभी सम्भव है जब सर्वशक्तिमान परमात्मा को स्वीकार कर लें, उसकी शरणागति की प्राप्ति हो जाय। मनुष्य रहते हुए मानवता की सीमा को भेदकर उसे देवस्वरूप में विकसित कर देना ईश्वर की शक्ति का कार्य है। उपासना का अर्थ परमात्मा से उस शक्ति को प्राप्त करना ही है।
जान-बूझकर या अकारण परमात्मा कभी किसी को दण्ड नहीं देता। प्रकृति की स्वच्छन्द प्रगति प्रवृत्ति में ही सबका हित नियन्त्रित है। जो इस प्राकृतिक नियम से टकराता है वह बार-बार दु:ख भोगता है और तब तक चैन नहीं पाता जब तक वापस लौटकर फिर उस सही मार्ग पर नहीं चलने लगता। भगवान् भक्त की भावनाओं का फल तो देते हैं किन्तु उनका विधान सभी संसार के लिये एक जैसा ही है। भावनाशील व्यक्ति भी जब तक अपने पाप की सीमायें नहीं पार कर लेता तब तक अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय रखते हुए भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता।
अपने से विमुख प्राणियों को भी वे दु:ख दण्ड नहीं देता दुख दण्ड देने के लिए शक्ति तो उसके विधान में ही है। मनुष्य का विधान तो देश, काल और परिस्थितियों वश बदलता ही रहता है। किन्तु उसका विधान सदैव एक जैसा ही है। भावनाशील व्यक्ति भी उसकी चाहे कितनी ही उपासना करे सांसारिक कर्त्तव्यों की अवहेलना कर या दैवी-विधाना का उल्लंघन कर कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसा कर्मबीज वैसा ही फल यह उसका निश्चल विधान है। दूसरों का तिरस्कार करने वाला कई गुना तिरस्कार पाता है। परमार्थ उसी तरह लौटकर असंख्य गुने सुख पैदाकर मनुष्य को तृप्त कर देता है। सुख और दु:ख, बन्धन और मुक्ति मनुष्य के कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। दुष्कर्मों का फल भोगने से मनुष्य बच नहीं सकता इस विधान में कहीं राई रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है।
अशुभ कर्मों का सम्पादन और देह का जड़ अभिमान ही मनुष्य को छोटा बनाये हुये है। शुभ-अशुभ कार्यों के फलस्वरूप सुख-दु:ख का भोक्ता न होने पर भी आत्मा मोह वश होकर दु:ख भोगती है। मैं देह हूँ ‘‘मुझे सारे अधिकार मिलने ही चाहिये’’ यह मान लेने से जीव स्वयं कर्त्ता-भोक्ता बन जाता है और इसी कारण वह ‘‘जीव’’ कहलाता है। जब तक वह इतनी -सी सीमा में रहता है तब तक उसकी शक्ति भी उतनी ही तुच्छ और संकुचित बनी ही रहती है। जब वह इस भ्रम रूप देहाध्यास का परित्याग कर देता है तो वह शिव-स्वरूप, ईश्वर-स्वरूप हो जाता है। उसकी शक्तियाँ विस्तीर्ण हो जाती हैं और वह अपने आपकों अनन्त शक्तिशाली, अनन्त आनन्द में लीन हुआ अनुभव करने लगता है।
अपनी तुच्छ सत्ता को परमात्मा की शरणगति में ले जाने से मनुष्य अनेकों कष्ट-कठिनाइयों से बच जाता है। गृहपति की अवज्ञा करके जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सुखी नहीं रह सकता उसी प्रकार परमात्मा का विरोधी भी कभी सुखी या सन्तुष्ट नहीं रह सकता। परमात्मा की अवमानना का अर्थ है उसके सार्वभौमिक नियमों का पालन न करना। अपने स्वार्थ, अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिये कोई भी अनुचित कार्य परमात्मा को प्रिय नहीं। इस तरह की क्षुद्र बुद्धि का व्यक्ति ही उसके कोप का भाजन बनता है पर जो विश्व-कल्याण की कामना में ही अपना कल्याण मानते और तदनुसार आचरण करते हैं। ईश्वर के अनुदान उन्हें उसी तरह प्राप्त होते हैं जैसे कोई पिता अपने सदाचारी, आज्ञा पालक और सेवा भावी पुत्र को ही अपनी सुख-सुविधाओं का अधिकांश भाग सौंपता है।
पापों का नाश हुये बिना, इन्द्रियों का दमन किये बिना, अन्त:करण की शुद्धि नहीं होती। संसार में रहते हुये मनुष्य कर्मों से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। अत: निष्काम कर्मयोग परमात्मा की प्राप्ति और सांसारिक सुखोपभोग का सबसे सुन्दर और समन्वययुक्त धर्म है। निष्काम भावनाओं में पाप नहीं होता वरन दूसरों के हित की, कल्याण की और सबको ऊँचे उठाने की विशालता होती है जिससे अन्त:करण की पवित्रता बढ़ती है और सुख मिलता है अतएव प्रत्येक मनुष्य को संसार समर का योद्धा बनकर ही जीवन यापन करना चाहिए। वह साहस वह गम्भीरता और वह कार्य करने की भावना मनुष्य ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म सान्निध्यता में ही प्राप्त करता है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i