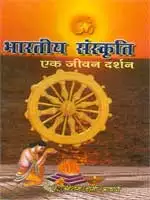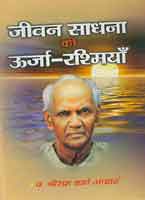|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> भारतीय संस्कृति एक जीवन दर्शन भारतीय संस्कृति एक जीवन दर्शनश्रीराम शर्मा आचार्य
|
13 पाठक हैं |
||||||
भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
संस्कृति का स्वरूप
आचरण के लिए विवश
करने वाली आस्था है। जिसका
अंतःकरण इस रंग में जितनी गहराई
तक रंगा हुआ है, वह उतना ही सुसंस्कृत है।
इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति के जीवन पर प्रकाश डाला गया है।
आचरण के लिए विवश
करने वाली आस्था है। जिसका
अंतःकरण इस रंग में जितनी गहराई
तक रंगा हुआ है, वह उतना ही सुसंस्कृत है।
इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति के जीवन पर प्रकाश डाला गया है।
भारतीय संस्कृति
जब कोई समाज कठिन से कठिन परस्थितियों में भी अपने व्यक्तिगत मान-अपमानों
की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि के अस्तित्व पर संकट या
संघर्ष में अपने प्राणों की बाजी लगाता है या फिर बलिदान हो जाता है, तो
वह व्यक्तिगत रूप से उस राष्ट्र और समाज की संस्कृति की ही रक्षा करता है
और बलिदान होना ही, उस बलिदानी वीर पुरुष की संस्कृति है।
यह संस्कृति ही है, जो राष्ट्र पर मर मिटने के लिए प्रेरित करती है और मर कर भी जब संतोष नहीं होता है, तो बलिदानी वीर पुरुष अगले जन्म में भी अपनी उसी मातृभूमि पर पैदा होकर अपने प्राणों को अपनी मातृभूमि के लिए अर्पित करने की ईश्वर से कामना करता है।
कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र और उसके नागरिकों के अस्तित्व के लिए संस्कृति उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितना कि उनके लिए भोजन हवा और पानी। जिस प्रकार भोजन, हवा और पानी के बिना कोई राष्ट्र और उसके नागरिक जीवित नहीं रह सकते उसी प्रकार बिना संस्कृति के राष्ट्र और नागरिकों का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है। इसलिए यह सत्यता है कि संस्कृति किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा भले ही न करती हो, पर राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा अवश्य करती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र और जाति की अपनी अलग-अलग संस्कृति होती है, उसी के अनुसार समाज, उस राष्ट्र और उस जाति की पहचान होती है।
आज संसार में यूरेनियम, अमरीकन, रूसी, चाइनीज, अरबी आदि अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, पर इस संसार के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि इनमें सबसे पुरानी संस्कृति भारतवर्ष की ही है।
साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ भी है, क्योंकि संसार की अन्य संस्कृतियों में अध्यात्मिकता का बहुत ही कम अंश पाया जाता है या अधिकांश आधिभौतिक विषयों तक ही सीमित है, पर भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति ही है, क्योंकि जो संस्कृति मनुष्य में ‘पंच तत्वों का पुतला’ होने की भावना भर दे और इस जीवन के बाद किसी प्रकार की आशा, भरोसा न दिला सके, वह मनुष्य या समाज की उन्नति कदापि नहीं कर सकती।
भारतीय संस्कृति ने आधिभौतिक अथवा लौकिक उन्नति की अवहेलना नहीं की है, जीवन को सुखी बनाने का मार्ग इसने स्पष्टता से समझाया है, पर अंतिम लक्ष्य सदैव आध्यात्मिक उन्नति को ही समझा है अथवा यह कहना चाहिए कि उसने समस्त लौकिक कार्यों और उद्योगों का संबंध आध्यात्मिक उन्नति से ही जोड़ दिया है, जिससे मनुष्य भौतिकवाद के दोषों से बच सके और समस्त सांसारिक कार्यों को करते हुए आत्मकल्याण के ध्येय को न भूले। अगर हमारी संस्कृति के निर्माताओं ने इस बात का ध्यान आरंभ से ही न रखा होता तो हमें भी वही दिन देखना पड़ता जो आज योरोप, अमरीका में दिखाई पड़ रहा है। वहाँ इस समय एक ओर भौतिक उन्नति और वैभव की पराकाष्ठा दिखलाई पड़ रही है, तो दूसरी ओर इतनी अधिकता पाई जाती है कि वे लोग किसी भी दिन अपने वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा आप ही नष्ट हो सकते हैं। इस अवस्था में उनकी रक्षा होगी तो वह भारतीय सभ्यता के सिद्धांतों (पंचशील) के अपनाने से ही संभव होगी है।
भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ अन्य देशों ने अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति का सर्वोच्च लक्ष्य सांसारिक सुख और भोग की सामग्री प्राप्त करना समझ रखा है, भारतवर्ष का लक्ष्य सदा त्याग का रहा है। दूसरों के भोगवाद के मुकाबले में हम यहाँ की संस्कृति का आधार त्यागवाद कह सकते हैं। अब यह स्पष्ट है कि जहाँ के मनुष्यों का लक्ष्य भोगवाद होगा वहाँ दूसरों से परस्पर संघर्ष चलता ही रहेगा, क्योंकि संसार में जितनी भोग-सामग्री है, उसके मुकाबले में मनुष्य की तृष्णा कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी है। ऐसी जातियों के व्यक्ति पहले विदेशी अथवा अन्य जाति के लोगों को लूटने-मारने का कार्य करते हैं और फिर जब बाहर का मार्ग रूक जाता है तो अपने ही देश के भाइयों पर हाथ साफ करने लगते हैं। उनके सामने कोई ऐसा आदर्श अथवा लक्ष्य नहीं होता, जिसके प्रभाव से वे ऐसे काम को बुरा समझें। उनको तो यही सिखाया गया है कि यह संसार सबलों के लिए है और यहाँ वही सफल मनोरथ होता है, जो सबसे अधिक शक्तिशाली या संघर्ष के उपयुक्त होता है।
इसके विपरीत भारतीय संस्कृति सिखलाती है कि इस संसार में जितनी वस्तुएँ दिखलाई पड़ती हैं, उनका महत्व बहुत अधिक नहीं है, वे क्षणभंगुर हैं और किसी भी समय नष्ट हो सकती हैं। वास्तविक महत्व की चीज आत्म-सत्ता या परमात्मत्त्व ही है, जो स्थायी और अविनाशी है। इसलिए मनुष्य को, जब तक वह संसार में है, भौतिक वस्तुओं का संग्रह और उपभोग तो करना चाहिए, पर अपनी दृष्टि सदा उसी सत्य आत्म-तत्त्व पर रखनी चाहिए, जो कि सब भौतिक वस्तुओं का मूल आधार है और जिसमें मनुष्य को-जीवात्मा को सदैव निवास करना है। इस भावना के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थन्ध होने से बचा रहता है और वह अपने हित के साथ दूसरों के हित की रक्षा का भी ध्यान रखने में समर्थ होता है। वह अन्याय और अत्याचारों के कार्यों से पाप समझ कर बचता है और इस प्रकार समाज में न्याय और सुख-शांति की स्थापना होती है।
यही कारण है कि भारतीयों ने सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करके भी कभी संसार बनाने की बात नहीं सोची और न कत्लेआम द्वारा किसी अन्य राष्ट्र का नामो-निशान मिटा देने का प्रयत्न किया। कोई समय ऐसा भी था कि संसार भर के धन का केंद्र भारत ही था और यहाँ सचमुच सोने और रत्नों के मंदिर और महल बनाए गए, पर उसने धन को अपना आदर्श कभी नहीं बनाया और उसके द्वारा अन्य देशों को अपने अधिकार में लाने की योजना कभी नहीं बनाई गई। सब प्रकार के सांसारिक वैभव को भोगते हुए भी उसने सदैव यह ख्याल रखा कि उसके ऊपर एक सत्ता उसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी। इसी आध्यात्मिक भावना के आधार पर उसका जीवन सदैव संयमयुक्त बना रहा और वह सब मनुष्यों को ही नहीं समस्त प्राणियों को एक ही परम पिता के बनाए मान कर, करूणा और प्रेम का पात्र समझता रहा।
भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता यह है कि इसका कभी एक समाज या श्रेणी विशेष से संबंध नहीं रहा। जैसे आजकल किसी देश की संस्कृति में पूंजीपतियों की ही प्रधानता है, किसी में मजदूरों का सिक्का लगा है, किसी में पुरातन पंथियों का जोर है तो नवपंथियों के सिर पर ही सेहरा बांधा जाता है, वैसी दशा भारतीय संस्कृति में किसी काल में नहीं रही। किसी एक प्रदेश में किसी राजा या धर्मध्वजा धारी ने अपने विरोधियों पर अत्याचार किए हों या किसी भाग को कुचल डाला हो तो यह तो दूसरी बात है, पर समस्त देश की दृष्टि से भारतीय संस्कृति में कभी कोई ऐसा विधान स्वीकार नहीं किया गया जिसके अनुसार एक समुदाय को तो सब प्रकार की सुविधाएँ और सुख मिले हों और दूसरे को भूखों मरने को छोड़ दिया गया हो। सच तो यह है कि यहाँ की संस्कृति में शोषण का सिद्धांत जो वर्तमान समय का मूल-मंत्र बना हुआ है, कभी स्वीकार नहीं किया गया और सदा ही घोषणा की गई-
यह संस्कृति ही है, जो राष्ट्र पर मर मिटने के लिए प्रेरित करती है और मर कर भी जब संतोष नहीं होता है, तो बलिदानी वीर पुरुष अगले जन्म में भी अपनी उसी मातृभूमि पर पैदा होकर अपने प्राणों को अपनी मातृभूमि के लिए अर्पित करने की ईश्वर से कामना करता है।
कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र और उसके नागरिकों के अस्तित्व के लिए संस्कृति उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितना कि उनके लिए भोजन हवा और पानी। जिस प्रकार भोजन, हवा और पानी के बिना कोई राष्ट्र और उसके नागरिक जीवित नहीं रह सकते उसी प्रकार बिना संस्कृति के राष्ट्र और नागरिकों का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है। इसलिए यह सत्यता है कि संस्कृति किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा भले ही न करती हो, पर राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा अवश्य करती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र और जाति की अपनी अलग-अलग संस्कृति होती है, उसी के अनुसार समाज, उस राष्ट्र और उस जाति की पहचान होती है।
आज संसार में यूरेनियम, अमरीकन, रूसी, चाइनीज, अरबी आदि अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, पर इस संसार के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि इनमें सबसे पुरानी संस्कृति भारतवर्ष की ही है।
साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ भी है, क्योंकि संसार की अन्य संस्कृतियों में अध्यात्मिकता का बहुत ही कम अंश पाया जाता है या अधिकांश आधिभौतिक विषयों तक ही सीमित है, पर भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति ही है, क्योंकि जो संस्कृति मनुष्य में ‘पंच तत्वों का पुतला’ होने की भावना भर दे और इस जीवन के बाद किसी प्रकार की आशा, भरोसा न दिला सके, वह मनुष्य या समाज की उन्नति कदापि नहीं कर सकती।
भारतीय संस्कृति ने आधिभौतिक अथवा लौकिक उन्नति की अवहेलना नहीं की है, जीवन को सुखी बनाने का मार्ग इसने स्पष्टता से समझाया है, पर अंतिम लक्ष्य सदैव आध्यात्मिक उन्नति को ही समझा है अथवा यह कहना चाहिए कि उसने समस्त लौकिक कार्यों और उद्योगों का संबंध आध्यात्मिक उन्नति से ही जोड़ दिया है, जिससे मनुष्य भौतिकवाद के दोषों से बच सके और समस्त सांसारिक कार्यों को करते हुए आत्मकल्याण के ध्येय को न भूले। अगर हमारी संस्कृति के निर्माताओं ने इस बात का ध्यान आरंभ से ही न रखा होता तो हमें भी वही दिन देखना पड़ता जो आज योरोप, अमरीका में दिखाई पड़ रहा है। वहाँ इस समय एक ओर भौतिक उन्नति और वैभव की पराकाष्ठा दिखलाई पड़ रही है, तो दूसरी ओर इतनी अधिकता पाई जाती है कि वे लोग किसी भी दिन अपने वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा आप ही नष्ट हो सकते हैं। इस अवस्था में उनकी रक्षा होगी तो वह भारतीय सभ्यता के सिद्धांतों (पंचशील) के अपनाने से ही संभव होगी है।
भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ अन्य देशों ने अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति का सर्वोच्च लक्ष्य सांसारिक सुख और भोग की सामग्री प्राप्त करना समझ रखा है, भारतवर्ष का लक्ष्य सदा त्याग का रहा है। दूसरों के भोगवाद के मुकाबले में हम यहाँ की संस्कृति का आधार त्यागवाद कह सकते हैं। अब यह स्पष्ट है कि जहाँ के मनुष्यों का लक्ष्य भोगवाद होगा वहाँ दूसरों से परस्पर संघर्ष चलता ही रहेगा, क्योंकि संसार में जितनी भोग-सामग्री है, उसके मुकाबले में मनुष्य की तृष्णा कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी है। ऐसी जातियों के व्यक्ति पहले विदेशी अथवा अन्य जाति के लोगों को लूटने-मारने का कार्य करते हैं और फिर जब बाहर का मार्ग रूक जाता है तो अपने ही देश के भाइयों पर हाथ साफ करने लगते हैं। उनके सामने कोई ऐसा आदर्श अथवा लक्ष्य नहीं होता, जिसके प्रभाव से वे ऐसे काम को बुरा समझें। उनको तो यही सिखाया गया है कि यह संसार सबलों के लिए है और यहाँ वही सफल मनोरथ होता है, जो सबसे अधिक शक्तिशाली या संघर्ष के उपयुक्त होता है।
इसके विपरीत भारतीय संस्कृति सिखलाती है कि इस संसार में जितनी वस्तुएँ दिखलाई पड़ती हैं, उनका महत्व बहुत अधिक नहीं है, वे क्षणभंगुर हैं और किसी भी समय नष्ट हो सकती हैं। वास्तविक महत्व की चीज आत्म-सत्ता या परमात्मत्त्व ही है, जो स्थायी और अविनाशी है। इसलिए मनुष्य को, जब तक वह संसार में है, भौतिक वस्तुओं का संग्रह और उपभोग तो करना चाहिए, पर अपनी दृष्टि सदा उसी सत्य आत्म-तत्त्व पर रखनी चाहिए, जो कि सब भौतिक वस्तुओं का मूल आधार है और जिसमें मनुष्य को-जीवात्मा को सदैव निवास करना है। इस भावना के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थन्ध होने से बचा रहता है और वह अपने हित के साथ दूसरों के हित की रक्षा का भी ध्यान रखने में समर्थ होता है। वह अन्याय और अत्याचारों के कार्यों से पाप समझ कर बचता है और इस प्रकार समाज में न्याय और सुख-शांति की स्थापना होती है।
यही कारण है कि भारतीयों ने सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करके भी कभी संसार बनाने की बात नहीं सोची और न कत्लेआम द्वारा किसी अन्य राष्ट्र का नामो-निशान मिटा देने का प्रयत्न किया। कोई समय ऐसा भी था कि संसार भर के धन का केंद्र भारत ही था और यहाँ सचमुच सोने और रत्नों के मंदिर और महल बनाए गए, पर उसने धन को अपना आदर्श कभी नहीं बनाया और उसके द्वारा अन्य देशों को अपने अधिकार में लाने की योजना कभी नहीं बनाई गई। सब प्रकार के सांसारिक वैभव को भोगते हुए भी उसने सदैव यह ख्याल रखा कि उसके ऊपर एक सत्ता उसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी। इसी आध्यात्मिक भावना के आधार पर उसका जीवन सदैव संयमयुक्त बना रहा और वह सब मनुष्यों को ही नहीं समस्त प्राणियों को एक ही परम पिता के बनाए मान कर, करूणा और प्रेम का पात्र समझता रहा।
भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता यह है कि इसका कभी एक समाज या श्रेणी विशेष से संबंध नहीं रहा। जैसे आजकल किसी देश की संस्कृति में पूंजीपतियों की ही प्रधानता है, किसी में मजदूरों का सिक्का लगा है, किसी में पुरातन पंथियों का जोर है तो नवपंथियों के सिर पर ही सेहरा बांधा जाता है, वैसी दशा भारतीय संस्कृति में किसी काल में नहीं रही। किसी एक प्रदेश में किसी राजा या धर्मध्वजा धारी ने अपने विरोधियों पर अत्याचार किए हों या किसी भाग को कुचल डाला हो तो यह तो दूसरी बात है, पर समस्त देश की दृष्टि से भारतीय संस्कृति में कभी कोई ऐसा विधान स्वीकार नहीं किया गया जिसके अनुसार एक समुदाय को तो सब प्रकार की सुविधाएँ और सुख मिले हों और दूसरे को भूखों मरने को छोड़ दिया गया हो। सच तो यह है कि यहाँ की संस्कृति में शोषण का सिद्धांत जो वर्तमान समय का मूल-मंत्र बना हुआ है, कभी स्वीकार नहीं किया गया और सदा ही घोषणा की गई-
‘‘आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न
समाचरेत्।’’
‘‘पर हित सरिस धर्म नहिं भाई।
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई।।’’
‘‘पर हित सरिस धर्म नहिं भाई।
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई।।’’
इस प्रकार सारे पदार्थ किसी खास आदमी या खास जाति के लिए नहीं बनाए हैं,
इसलिए न्यायनुसार उन पर मनुष्य मात्र का समान अधिकार है। भूमि, जल, हवा,
समुद्र आदि प्रकृतिप्रदत्त पदार्थों पर किसी व्यक्ति के द्वारा एकाधिकार
जमाने की चेष्टा पर बड़ा भारी जुर्म या परमात्मा के खिलाफ बगावत की तरह
माना जाता था। हमारा अनुमान है कि आज कल के साम्राज्यवादियों या
पूंजीवादियों की तरह प्राचीनकाल में रावण और कंस आदि इसी विचार धारा के
मनुष्य थे। इसी कारण उनको राक्षस की पदवी दी गई है और जनता-जनार्दन ने
उनके नाश की मांग की, जो परमात्मा द्वारा शीघ्र ही पूर्ण की गई। भारतीय
विचारकों ने ऐसे अस्वाभाविक सिद्धांतों की जड़ ही यहाँ न जमने
दी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i