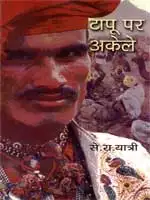|
सामाजिक >> टापू पर अकेले टापू पर अकेलेसे. रा. यात्री
|
436 पाठक हैं |
|||||||
‘टापू पर अकेले’ उपन्यास एक ऐसे समाज-विमुख व्यक्ति की कथा है जो अपने सोच, पसन्द और दृष्टिकोण में किसी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं समझता।
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
‘टापू पर अकेले’ उपन्यास एक ऐसे समाज-विमुख व्यक्ति
की कथा है जो अपने सोच, पसन्द और दृष्टिकोण में किसी से जुड़ने की
आवश्यकता नहीं समझता। निदान वह अपने सामाजिक परिवेश से असम्पृक्त होते चले
जाने की स्थिति में सब तरफ से कटकर अकेला रह जाता है।
सामन्ती परिवेश के छिन्न-भिन्न होने की स्थिति में ‘टापू पर अकेले’ उन पात्रों की कथा है जो नए जीवन के सन्दर्भों में अपनी प्रासंगिकता तलाश करने में जुटे हैं, किन्तु पुरानी पड़ती पीढ़ी का पात्र कुँवर वीरेन्द्र सिंह घोर अतीतजीवी प्राणी है जो जीवन की केन्द्रीय धारा से कटकर एक सूखी नदी अथवा मरुस्थल में बदल जाता है।
लेखक ने इस त्रासद कथा की विषमता और संकट को आधुनिक भाषा और मुहावरा देकर अत्यन्त जीवन्त रूप में प्रस्तुत किया है।
सामन्ती परिवेश के छिन्न-भिन्न होने की स्थिति में ‘टापू पर अकेले’ उन पात्रों की कथा है जो नए जीवन के सन्दर्भों में अपनी प्रासंगिकता तलाश करने में जुटे हैं, किन्तु पुरानी पड़ती पीढ़ी का पात्र कुँवर वीरेन्द्र सिंह घोर अतीतजीवी प्राणी है जो जीवन की केन्द्रीय धारा से कटकर एक सूखी नदी अथवा मरुस्थल में बदल जाता है।
लेखक ने इस त्रासद कथा की विषमता और संकट को आधुनिक भाषा और मुहावरा देकर अत्यन्त जीवन्त रूप में प्रस्तुत किया है।
1
कई बीघे का रकबा पार करके चहारदीवारी से लगे इस ऊबड़-खाबड़ ढंग से बने
कमरे के दरवाज़े पर जाकर मैं थोड़ी देर चुपचाप खड़ा भीतर की टोह लेता रहा।
हमेशा यही होता था। उसके कमरे में तीन तरफ दरवाज़े थे और वह कभी बन्द नहीं होते थे, पर भीतर की सुनगुन बाहर खड़े व्यक्ति को शायद ही कभी मिल पाती हो। पता नहीं वह भीतर बैठा क्या करता रहता था ? कोई भी हो, क्या वह लम्बे वक्त तक महज दिवास्वप्नों में खोया रह सकता है ?
मैंने कुछ पलों के लिए अपने हाथ में लटका सूटकेस दहलीज पर टिका दिया था। जब भीतर से कोई आहट सुनाई नहीं पड़ी तो मैंने उसे उठाया और सोचा, फालतू में कयास लगाने में वक्त क्यों गँवाया जाए। कुछ खास तो वह कर नहीं रहा होगा-सीधे चलकर देख ही लिया जाए !
अभी चारेक दिन पहले मुझे उसका एक अन्तर्देशीय मिला था। वह चाहता तो दो-ढाई पंक्तियों के लिए एक कार्ड भी लिख सकता था। पर नहीं, फालतूपन से उसे कोई परहेज़ नहीं था। चींटे की टाँगों सरीखी लिखावट में उसने घसीट रखा था कि जरूरी सलाह-मशविरा करना है-इसे खास अहमियत दो।
मेरे पहुँचने पर जोर देने का यों कोई खास अर्थ नहीं था, क्योंकि मैं उसके स्वभाव से परिचित था। वह बहुत काहिल और आत्मकेन्द्रित व्यक्ति था। शायद सारी दुनिया में मैं ही एकमात्र वह शख़्श था जिसे वह भूले-भटके कभी पत्र लिखता होगा। उसका खत पाने के बाद मैं देर तक इस बात पर विचार करता रहता था कि उसने खत-लिफाफा या अन्तर्देशीय कैसे और कहाँ से प्राप्त किया होगा। वह तो अपने कोठड़े से निकलकर पोस्ट ऑफिस तक जाने से रहा। किसी ने खत लाकर दिया भी होगा तो कितने दिनों बाद उसे लिखने की नौबत आई होगी और फिर वह उसकी मेज पर इस प्रतीक्षा में बेचैन पड़ा रहा होगा कि उसकी उस जेलखाने से किसी प्रकार मुक्ति तो हो। उसके खत के सिरनामे पर कोई पता या तारीख अंकित नहीं होती थी। उसके खत बस इस बात के परिचायक होते थे कि वह किसी गहरे मानसिक द्वन्द्व से बाहर नहीं निकल पा रहा है।
उपरोक्त विवरण से आप यह न समझें कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात कह रहा हूँ जो मामूली पढ़ा-लिखा ऐसा अभिव्यक्ति विमुख जीव है जो लिखना-पढ़ना ही न जानता हो। वह उन्नीस सौ अड़तीस का सेन्ट जॉन्स कॉलेज का लॉ ग्रेजुएट था। पढ़ाई के बाद कुछ वर्ष यूरोप में भी घूम चुका था। मगर उसने कभी कोई काम हाथ में नहीं लिया था। यहाँ तक कि वकालत का लाइसेन्स लेने के बावजूद एक दिन के लिए भी किसी मुवक्किल के मुकद्दमे की पैरवी करने के लिए कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ था। हाँ, यह दीगर मुद्दा है कि परिवारी जमीन-जायदाद के मामले-मुकद्दमों में वह यदा-कदा कचहरी चला जाता था। जो उससे सलाह लेने आते थे उन्हें कानूनी दाँव-पेंच भी खूब समझा देता था।
उसका नाम कुँवर वीरेन्द्र बहादुर सिंह था। मगर मैं अथवा कोई पुराना दोस्त उसे सिर्फ कुँवर कहकर सम्बोधित करते थे। मैं अन्त तक उसका सहपाठी नहीं रह गया था। मैं मैट्रिक में उसके साथ था और बाद में वह बाहर पढ़ने चला गया था। हाई स्कूल में पढ़ते हुए भी वह फोर्ड गाड़ी में स्कूल आता था। यह उस दौर की बात है जब मेरे जैसे निम्न-मध्यवर्गीय परिवारों के विद्यार्थी पैदल चलकर ही स्कूल पहुँचते थे। बहुत हुआ तो कोई भाग्यशाली साइकिल पा जाता था। साइकिल की कीमत दस-पन्द्रह रुपये से अधिक नहीं थी, मगर वह-पन्द्रह भी किसको मयस्सर होते थे ?
मैंने दरवाज़े से चार-छह कदम आगे बढ़कर देखा कि कमर के पीछे दोनों हाथ बाँधे खोयेपन की मनःस्थिति में एक तख्त के इर्द-गिर्द चक्कर काट रहा है। जब मैंने पाया कि वह दरवाज़े से भीतर दाखिल होने वाले के अस्तित्व से पूरी तरह बेखबर है तो मैंनें आगे बढ़कर अपना सूटकेस तख्त पर टिका दिया।
मुझे अपने सामने देखकर वह ठहर तो गया पर उसके लम्बे-चौड़े मस्तक पर खिचीं अनगिनत रेखाएँ यथावत् बनी रहीं। आँखें उसी तरह चढ़ी हुई उसकी तुनकमिजाजी का हवाला देती रहीं। एक बहुत पुराना फौजी ओवरकोट उसकी तीन-चौथाई देहयष्टि को ढँके हुए था और कोट के कालर गर्दन को छिपाए हुए थे।
वह मुझसे कुछ नहीं बोला तो मैं आगे बढ़कर उसकी लम्बी-चौड़ी मसहरी की पाटी पर टिक गया। मैं उसकी इस तरह की कदीमी मनहूसियत से बाखबर था इसलिए मेज पर रखी सिगरेट की डिब्बी और लाइटर उठाकर सिगरेट जलाने में लग गया। उसने मुझे सिगरेट का लम्बा कश खींचते देखा और फिर चक्कर काटने लगा। मैंने जूते उतारे और पलँग पर पसर गया। उसके कमरे पर टीन की चादरें पड़ी थीं और सहन में खड़े नीम की पत्तियाँ टीन की छत पर गिरकर हल्की खड़क पैदा कर रही थीं।
मैंने स्वयं को हल्का छोड़ दिया और उसको उसके हाल पर चलने दिया। जब उसका जी भर जाएगा या चक्कर काटते-काटते पाँव थक जाएँगे तो वह स्वयं ही कुछ न कुछ बोलने लगेगा। ऐसे सिरफिरे आदमी को क्या कहा जाए जो अपने दोस्त को पत्र लिखकर तुरन्त चले आने का अनुरोध करता है और उसके आ जाने पर उससे फूटे मुँह कुछ बोलता-कहता तक नहीं है।
मैंने सिगरेट के कई लम्बे-लम्बे कश लिए और धुआँ ऊपर छत की ओर छोड़ते हुए करवट बदल ली और कुँअर के बारे में ही सोचने लगा।
कुँवर का पारिवारिक आवास एक किले सरीखा है जिसमें पैंतालीस-पचास छोटे बड़े कमरे, कोठरियाँ और दीवानखाने हैं। उस पूरी हवेली का एक बार जायजा लिया जाए तो दो घंटे से कम नहीं लगेंगे। दूर-दूर तक उस आवास को लाल हवेली के नाम से जाना और पुकारा जाता है। झिर्रियों और झिलमिली वाली खिड़कियों और दरवाजों से लैस तथा मेहराबों और कँगूरों से आवृत वह हवेली कम से कम दो सवा दो सौ साल पुरानी तो जरूर ही रही होगी। कस्बे के इस पुरातन भवन को भीतर से देखने की उत्कण्ठा कस्बे के बाशिन्दों की हसरत जैसी है। कुँअर ने उस हवेली के अन्तरंग से अपना सम्बन्ध बरसों पहले ही तोड़ लिया है और चहारदीवारी के अन्तिम छोर पर एक लम्बा-चौड़ा अनगढ़-सा कोठड़े बनवाकर पड़ा हुआ है। कोठड़े की बाजू में एक छोटी-सी कोठरी भी डलवा ली है जो मैंने पिछली बार नहीं देखी थी।
कस्बे की हवेली के अलावा बस्ती से कोई तीनेक मील के फासले पर सीकरी मौजे में भी एक किलानुमा गढ़ी है। वह तो शायद तीन सौ साल पुरानी होगी। कई एकड़ जमीन पर आबाद उस हवेली के सदर दरवाज़े के ऊपर जो मशाल जलती है उसे दूर-दूर तक के इलाके में देखा जाता है। पर ऐसे मौके अब गिने-चुने ही रह गए हैं, क्योंकि राजा हीरासिंह के देहावसान के बाद सीकरी में बरसों से कोई नहीं रहता। सौ-सवा सौ कमरों, बारादरियों, दीवानखानों वाली गढ़ी उपेक्षित पड़ी है। कुँवर वीरेन्द्रबहादुर के नाना राजा हीरासिंह कोठी के आखिरी उत्तराधिकारी थे। उन्होंने ही अपनी बड़ी बेटी और उसके बेटों को अपने संरक्षण में बुला लिया था और अपनी देख-रेख में उनकी परवरिश की थी। पूरे इलाके में राजा हीरासिंह का दबदबा था और आले दर्जे के हाकिम-हुक्काम आए दिन सीकरी में दिखाई पड़ते रहते थे। राजा साहब नाच-गाने और शिकार के जबरदस्त शौकीन थे। नाच-गानों के जश्न तो होते ही रहते थे-अंग्रेज अफसरों की अगवानी के अवसर पर तरह तरह के जश्न भी मनाए जाते थे। नौबतखाने में दस-बारह हाथी और घुड़साल में सौ-सवा सौ असली नस्ल के घोड़े खड़े हिनहिनाते रहते थे।
सीकरी के आसपास लगे सैकड़ों गाँवों में राजा हीरासिंह की रैयत फैली पड़ी थी। राजा हीरासिंह अपने पुरखों की ग्यारहवीं पीढ़ी के नौनिहाल थे। जिस समय उस गढ़ी का निर्माण हुआ था, अंग्रेजों के पाँव इस देश में पूरी तरह नहीं फैले थे। वह देशी राजे-रजवाड़ों का युग था और प्रत्येक प्रान्त में इस तरह के राव-राजे-सामन्त बिखरे पड़े थे। किसी को भी आज सीकरी के उस विशाल भवन को देखकर सहज ही आश्चर्य होगा, क्योंकि धुर देहात में उस तरह के निर्माण में जो श्रम और बुद्धि लगानी पड़ी होगी वह चकित करने वाली रही होगी।
जब मैं कुँवर के साथ पढ़ता था तो उसकी मेरे से अच्छी रब्त-जब्त हो गई थी। वह अपने वैभव में बेजोड़ था तो मैं अपने अभावों का जीता-जागता नमूना था। शायद वैभव भी कभी-कभी निर्धनता को देखकर चमत्कृत होता है और उसकी ओर हठात् खिंचता चला जाता है। कहाँ वह फोर्ड गाड़ी में ब्रीचेस और पम्पशू डाटकर आने वाला जैंटिलमैन और कहाँ मैं सूती कमीज और उठंग पाजामा पहनकर आने वाला निरीह-सा विद्यार्थी ! तीन या चार आने की जो सस्ती सी चप्पलें पहनकर मैं स्कूल पहुँचता था उन पर निगाह जाते ही मेरी विपन्नता का विराट स्वरूप सामने आ जाता था।
एक बार कुँवर मुझे बग्घी में अपने साथ बिठाकर सीकरी की उस आतंक जगाने वाली गढ़ी में ले गया था। मैं लम्बे-चौड़े रकबे में फैली उस इमारत में खो सा गया था। इधर-उधर घुमाने के बाद राजा हीरासिंह का दीवान मुझे एक बहुत बड़े हॉल में ले गया था। उस दीवानखाने की दीवारें बहुत ऊँची और छत झाड़-फानूसों से भरी हुई थी। मैंने सारी दीवारों पर हीरासिंह के वंश-वृक्ष की बड़ी-बड़ी आदमकद तस्वीरें स्वर्णाभ चौखटों में जड़ी देखी थीं। उन पुरखों की लम्बी-चौड़ी आकृतियाँ देखकर मन में सहसा एक विचित्र-सा आतंक पैदा हो जाता था।
गढ़ी नदी के बाएँ किनारे पर स्थिति थी। लम्बी-चौड़ी छतों से देखने पर नदी का महत्त्व और सुन्दरता समझ में आ जाती थी। यही-नहीं, उस विशाल गढ़ी में कई दीवानखाने थे। सभी बड़े कमरों की छतें भारी-भारी झाड़-फानूसों से सजी हुई थीं। छतों के कुंदों में कई स्थानों पर रंग-बिरंगे गोल-गोल हंडे भी लटके हुए थे। तरह-तरह की मूर्तियाँ और संगमरमर की छतरियाँ यहाँ-वहाँ देखी जा सकती थीं। लम्बे-चौड़े जलाशय और बागों में फव्वारे तो सब जगह नजर आते थे। पत्थरों के घाटों वाले सरोवर और स्फटिक-सा स्वच्छ उनमें भरा नीला जल मन को अनायस मोह लेता था।
यह सब भी तब तक बहुत पुराना हो चुका था। गढ़ी का वैभव और चहल-पहल राजा हीरासिंह के जीवित रहने की अवधि में ही निष्प्रभ होने लगी थी। मैं जब कई दशक पहले कुँवर के साथ वहाँ गया था तब तक कितने ही दास-दासियाँ वहाँ से विदा हो चुके थे और रनिवास भी सन्नाटे में डूबा हुआ था।
अब तो शायद बूढ़ा दीवान भी मर चुका था और सीकरी की हवेली पूरी तरह से निर्जन हो गई थी। वहाँ किसी के बने रहने की स्थितियाँ धीरे-धीरे दुर्वह होती चली गई थीं।
कुँवर के कस्बे से बाहर चले जाने पर मेरा उसके परिवार और सीकरी की गढ़ी से सम्बन्ध लगभग टूट ही गया था। कभी-कभी मैं कस्बे के बाजार में राजा हीरासिंह की गाड़ी खड़े देखता था। अंग्रेज बहादुर के रंग में रँग जाने के बाद उन्होंने अपने हाथी-घोड़े बेच दिए थे और अपनी फोर्ड पर ही शहर आते थे। उस गाड़ी को वह स्वयं ही चलाते थे। उनकी छत विहीन फोर्ड को हर कोई पहचानता था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह हाट-बाजार में चालू हालत में खड़ी रहती थी और उसके मडगार्ड बराबर हिलते रहते थे। कस्बे की लाल हवेली के बाहर तो वह गाड़ी अक्सर खड़ी ही रहती थी।
राजा हीरासिंह की देह गुलाबी गोरापन लिए हुए थी और उनकी आँखें नीले काँच की गोलियों सरीखी नज़र आती थीं। उनके सिर पर खाकी रंग का हैट होता था। खाकी बिरजेस और खुले कालर वाले कोट में वह अपने रूप-रंग से बजाय राजा के किसी अंग्रेज सार्जेण्ट जैसे दीख पड़ते थे।
बुढ़ापे के दिनों में राजा हीरासिंह के हाथ-पैर ही क्या बल्कि सारा शरीर ही हिलने लगा था। मैंने उन्हें कितनी ही दफा बीच सड़क में मोटर रोककर कस्बे के लोगों से बतियाते देखा था। राजा का खिताब पाने के बाद भी उनमें कोई राजसी ठसक दिखाई नहीं पड़ती थी। वह जनसाधारण से भी एक सहज-सरल बुजुर्ग की तरह पेश आते थे। इधर उनके हाथ और सिर हिलता रहता था उधर-मोटर के इंजन के चालू होने की वजह से उसकी भी बाँडी काँपती-काँखती रहती थी। मोटर और उनकी स्थिति समान हो चली थी-गोया मोटर भी उनकी तरह की पार किन्सन रोग से ग्रस्त हो गई थी।
राजा हीरासिंह की पाटदार आवाज़ में भी कंप का स्पष्ट आभास मिलता था। बहुत बाद में जब बोलती फिल्में हमारे कस्बे के सिनेमाहॉल में दिखाई जाने लगीं तो मैंने राजा हीरासिंह की शक्ल-सूरत से मिलता-जुलता एक अभिनेता देखा था। बाद में पता चला कि उसका नाम चन्द्रमोहन था।
लोगों का खयाल था कि राजा हीरासिंह अचूक निशानेबाज थे। बुढ़ौती में भी वह अंग्रेजों और देशी हुक्कामों के साथ खूब सैर-सपाटों पर जाते थे और शिकार में तो खास तौर से सम्मिलित रहते थे। यह कभी नहीं हुआ कि उनकी बन्दूक की नली से निकली गोली व्यर्थ गई हो।
राजा हीरासिंह जी की मौज-मस्ती, ऐश और अय्याशी में तीन-चौथाई जायदाद तो उनके सामने ही बिक चुकी थी। जो रेहन रखी गई थी वह भी कभी नहीं छुड़ाई जा सकी। पर एक बात ऐसी थी कि जिसमें कभी कोताही नहीं हुई-राजा साहब अधिक-से-अधिक समय अपनी सीकरी की गढ़ी में ही बिताते थे। कुँवर वीरेन्द्रबहादुर सिंह और उनके बड़े-भाई कुँवर रामपाल सिंह का परिवार भी यदा-कदा सीकरी जाता रहता था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कुँवर लोगों तथा उनके परिवारों का सीकरी जाना तभी तक सम्भव हो पाया जब तक राजा हीरासिंह जीवित रहे। चूँकि उनकी पत्नी का देहान्त चालीस-पैंतालीस की उम्र में ही हो चुका था और उनकी एकमात्र सन्तान वह बेटी ही थी जिसके बेटे कुँवर बीरेन्द्रबहादुर और कुँवर रामपाल सिंह थे। इसलिए बाद में गढ़ी एक तरह से खाली ही पड़ी रह गई। शहर या कस्बे की कोई इमारत होती तो उसकी अच्छी कीमत लग जाती, मगर गाँव में उस महल को कोई क्यों खरीदता ? बस बाद में एक-दो नौकर-चाकर या पुराने कारिन्दे ही उसमें रहते रहे।
मैं पुरानी यादों में डूबा हुआ था और यह बिल्कुल भूल चुका था कि मैं कुँवर बीरेन्द्रबहादुर के कोठड़े में उनके पलँग पर पड़ा दिवास्वप्न ले रहा हूँ। तभी कोई धम्म से टीन की छत पर कूदा। इसके कई मिनट बाद तक धम-धम की आवाजें होती रहीं तो मैं पलँग से उठा और सामने वाले दरवाज़े से बाहर निकल गया। बन्दरों की पूरी फौज नीम के पेड़ से कूद-कूदकर छत पर इकट्ठी हो गई थी।
मैं कमरे में वापस लौटा तो मैंने कुँवर को बदस्तूर चक्कर काटते देखकर मुस्कराते हुआ कहा, ‘‘कुँवर बहादुर को लंका जीतने का न्यौता देने के लिए पूरी वानर सेना छत पर सजी बैठी है।’’
कुँवर मेरा व्यंग्य सुनकर ठहर गया और आँखें माथे पर चढ़ा लीं। उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला-जैसे वह एकदम गूँगा-बहरा हो गया। पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा था कि वह अजीब-खब्ती जैसा होता चला जा रहा था। हँसना किस चिड़िया का नाम होता है यह तो वह जैसे भूल की चुका था। मैंने दिमाग पर जोर देकर बहुत सोचा कि मैंने उसे पिछली बार हँसते या मुस्कराते कब देखा था-पर मुझे वह अवसर याद नहीं आया। घर-परिवार को लेकर उसे कितनी गहरी विरक्ति हो चली थी इसका अनुमान तो बस इसी बात से लगाया जा सकता था कि वह चहारदीवारी में ही खड़ी हवेली की ओर कभी झाँकता भी नहीं था। एक नौकर इस टीन शेड में दोनों समय का खाना पहुँचा जाता था। उसकी जिन्दगी का एक दिन नज़दीक से देख लेने मात्र से उसकी जीवनचर्या को बखूबी समझा जा सकता था। वह एक अजीब मनहूस और अजनबियत-भरी जिन्दगी जी रहा था-जिसे सन्दर्भों से कटी हुई और पूरी तरह अप्रासंगिक कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं मानी जानी चाहिए।
आपने ऐसी कोई नीरस कहानी अवश्य पढ़ी या सुनी होगी जिसमें महज एक आदमी होता है जो कमरे में बैठा या इधर-उधर टहलता रहता है। सिगरेट के बाद सिगरेट फूँकता चला जाता है। इसके अलावा वहाँ कुछ भी उल्लेखनीय घटित नहीं होता। कमरा धुएँ के घोट से घुटता रहता है और वह मनहूस आदमी उसमें घुटकर खाँसता या काँखता रहता है। शायद आपने ऐसी कहानी न भी पढ़ी या सुनी हो, मगर यह इस जीवन और दुनिया की एक त्रासद सच्चाई है कि ऐसा होता है और इस पृथ्वीतल पर ऐसे न जाने कितने पात्र हैं जो व्यर्थता की भूमिकाओं में साँस ले रहे हैं। जब भी मैं कुँअर को देखता था मुझे उपरोक्त नीरस कहानी एकदम सच्ची और अपने सामने घटित होती दिखाई पड़ने लगती थी।
अपने परिचय और अन्तरंग दायरे में मैंने कुँअर जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं देखा। सुबह उठकर बिजली के चूल्हे पर वह अपनी चाय खुद तैयार करता था। चूँकि उसका कोठड़ा पिछले गेट के नजदीक पड़ता था, इसलिए वह दरवाज़े के सामने की गली से गुजरने वाले किसी भी आदमी या लड़के-बाले को पकड़ बुलाता और अपनी आवश्यकता का सामान उससे मँगवा लेता था। सारा कस्बा राजा हीरासिंह के धेवतों के रौब-दाब से परिचित था, इसलिए उस परिवार के छोटे-मोटे कामों को पूरा करने के लिए हर कोई खुशी से तैयार हो जाता था। सामन्ती दबदबा तो उस वक्त तक इस कदर दम तोड़ चुका था कि किले सरीखी लाल हवेली की बरसों तक सफाई-पुताई भी सम्भव नहीं हो पाती थी। लम्बे समय की अय्याशी, काहिली और परोपजीवी बने रहने की मानसिकता ने सबको आरामतलबी और जड़ता की जंजीरों में जकड़कर रख दिया था। बड़े कुँवर रामपाल सिंह न जाने कितनी कम्पनियों के मैनेजिंग डॉयरेक्टर के साथ-साथ और भी न जाने क्या-क्या थे। मगर अपनी सामन्ती ठसक में कहीं से कुछ कमाने के बजाय बड़े आदमियों को अपनी हवेली में पार्टियाँ देने के चक्कर में अपनी गाँठ का ही बहुत कुछ गँवा देते थे। लगता था जैसे वह सहज अपने बड़प्पन को बनाए रखने के उद्देश्य से ही सभा-सम्मेलनों और कम्पनियों से जुड़े रहते थे।
दोनों कुँवरों के बेटे-बेटियाँ बाहर के बड़े शहरों में हॉस्टलों में रहकर महँगी पढ़ाई कर रहे थे। कुँवर वीरेन्द्र सिंह का बड़ा बेटा रेलवे इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी करके कलकत्ता में अप्रेन्टिसशिप का कार्यकाल पूरा कर रहा था और कुँवर रामपाल सिंह का बेटा इंजीनियर्स इंडिया में कार्यरत था। इन दोनों लड़कों में से कभी कोई अपनी जन्मभूमि यानी उनींदे कस्बे में आना तथा लाल हवेली में रहना गवारा नहीं करता था। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी दरबारी संस्कृति के प्रति उन्हें किसी प्रकार का लगाव नहीं था, बल्कि यह कहना ज्यादा सच होगा कि उन्हें सामन्ती रखरखाव के प्रति घोर वितृष्णा थी।
कुँवर परिवार के पास कितने ही गाँवों की सम्पत्ति थी पर उन्होंने जमीन को कभी हाथ नहीं लगाया था। खुद काश्त न होने की वजह से लगभग सारा इलाका उनके हाथ से निकल चुका था। जमींदारी की सम्पत्ति की घोषणा के बाद उन्हें जो भी मुआवज़ा मिलता था वह ऊँट के मुँह में जीरा की कहावत को अक्षरशः चरितार्थ करता था। अभी भी कस्बे की पुरानी जायदादें बेचकर ही रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की जा रही थीं। कभी-कभी तो यह तक भी होता था कि घर का कोई पुराना खैरख्वाह चुपके से हवेली में बुलाया जाता था और बड़ी कुँवरानी (कुँवरों की माँ हीराबेन) कोई जेवर या जवाहरात उसको सौंपकर किसी दूसरे शहर में बिकवाती थी और इस प्रकार घर-परिवार की ठप्प होती गति को संचालित करती थी।
मैं जब पिछली बार हवेली में आया था तो मुझे कुँवर रामपाल सिंह ने बतलाया था कि कुँवर वीरेन्द्र सिंह अपने हिस्से का मुआवजा खुद ही वसूल करता था। उसने पूरे परिवार की बिगड़ती स्थिति की ओर से पूरी तरह आँखें मूँद ली थीं। दिन छुपते ही शराब की पूरी भरी बोतल लेकर बैठ जाता था। जब बोतल खत्म हो जाती थी तो सदर दरवाज़े पर जाकर खड़ा हो जाता था और नशे की हालत में सड़क से गुजरते किसी को भी बुलाकर देसी शराब के ठेके से सस्ती शराब की बोतल मँगवा लेता था।
कुँवर रामपाल सिंह के कथन की सच्चाई मैंने कुँवर वीरेन्द्र सिंह के कमरे में घुसते ही भाँप ली थी। उसके पलँग के नीचे अंग्रेजी और देसी शराब की खाली बोतलों का अंबार लगा हुआ था।
बहुत पहले जब कुँवर ने कानून की पढ़ाई पूरी की थी तो उसकी सेहत देखने के काबिल थी। उसके कद्दावर और संतुलित शरीर को देखकर किसी को भी ईर्ष्या हो सकती थी। पर अब उसे देखकर तरस आता था। उसका चेहरा काला पड़ गया था। स्वास्थ्य इसी सीमा तक चौपट हो चुका था कि वह महज एक लम्बा-चौड़ा ढाँचा भर रह गया था।
उससे लम्बे समय की यारी-दोस्ती थी इसलिए मेरा उसके पास पहुँचना किसी समय-विशेष का मोहताज नहीं था; बाकी तो दिन छिपने के बाद उसे अपने कमरे की दहलीज पार करने वाले पर इतना गुस्सा आता था कि वह कुछ भी कर सकता था। किसी तरह हम दोनों की राह-रस्म बस निभती ही चली आ रही थी, क्योंकि सारा लोक-व्यवहार लँगड़ा और पूरी तरह इकतरफा था। वह स्वयं तो इस सीमा तक आत्मकेन्द्रित था कि किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता था। वह बहुत कुछ पशु-प्रवृत्ति से ग्रस्त हो चला था।
अक्सर तो उसके कोठड़े के दरवाज़े साँझ होते ही बन्द हो जाते थे। कोई भूले-भटके उसके दरवाज़े पर दस्तक दे भी देता तो वह कड़ककर पूछता, ‘कौन ?’ यही नहीं ‘कौन’ बोलने के साथ ही वह पलँग पर पड़ी भरी बंदूक उठाकर खड़ा हो जाता था। उसके इस प्रकार के आवेश-भरे व्यवहार पर कभी-कभी मैं हँस भी पड़ता था। मेरे चेहरे पर हँसी देखकर वह अपने होंठ चबाने लगता था। एक बार तो टिन शेड की बगल में खड़े लहीम-शहीम नीम के पेड़ पर कुछ हलचल की आहट पाते ही उसने बाहर जाकर बन्दूक दाग दी। बाद में पाया गया कि कोई भी हादसा नहीं गुजरा। नीम पर बैठा एक बन्दर धाँय की आवाज़ से डरकर टिन पर गिर पड़ा और साथ ही नीम की एक बड़ी-सी शाख टूटकर टिन की छत पर आ गिरी। संयोग से इस हास्यास्पद घटना के समय मैं उसके कोठड़े में मौजूद था। मगर मेरे ठठाकर हँसने के बावजूद उस पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। वह नशे में गलतान था और चेहरा तना, आँखें हमेशा की तरह कपाल पर चढ़ी हुई थीं। उसके भीतर जो बेचैनी का तूफान उमड़ता रहता था उसे वह कोठड़े में चक्कर काटकर ही सहन करता था। उसे यों घूमते, चक्कर काटते देखकर यही अहसास होता था जैसे कोई घायल पशु तकलीफज़दा हालत में अपने बाड़े में घूम-फिर रहा हो।
ऐसा भी कई बार होता था कि मैं उसके पास पहुँचने के अवसर टालता चला जाता था। ऐसी स्थिति में मुझे उसका तार मिलता था : समथिंग इम्पार्टेण्ट टु बी डिसकस्ड (आवश्यक मुद्दे पर विचार-विमर्श)।
अगर मैं तार की भी परवाह नहीं करता था तो वह मुझे नाराज़ खयाल करता था और बैरंग खत भेज देता था। जब उसके पास पहुँचता था, प्रायः शाम या रात हो जाती थी। अपनी पूरी सख्ती और तने हुए चेहरे के बावजूद वह मुझे बहुत निरीह, दयनीय और टूटा हुआ नज़र आता था। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती थी तो मैं नाराज होकर कहता था, ‘कुँवर, उस जहर पर काबू करो, ये तुम्हें ले बैठेगा। क्या हिकारत के अलावा तुम्हारी जिन्दगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है ?’
मुझे खुश करने की नीयत से वह दोनों कानों पर हाथ रखकर आगे कभी न पीने की तौबा करता था-शराब को भद्दी-भद्दी गालियाँ देता था। उसकी इस हरकत पर मुझे हँसी आने लगती थी। मैं उसकी भावुकता और ऐसे हवाई वायदों को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। यह बात मुझसे छिपी नहीं थी कि यह सब रात-भर का कौल करार है, दिन निकलते ही उसकी सारी विनम्रता और भावुकता हवा हो जाएगी। वह हमेशा की तरह वही पुराना कुँवर-सागर-तट पर फैली बालू जैसा शुष्क और किरकिरा हो उठेगा।
मैंने पिछली घटनाओं से उबरते हुए सिगरेट की डिब्बी से एक सिगरेट खींची और लाइटर से जलाकर नाक और मुँह से खिलन्दड़ेपन से धुआँ छोड़ने लगा।
हमेशा यही होता था। उसके कमरे में तीन तरफ दरवाज़े थे और वह कभी बन्द नहीं होते थे, पर भीतर की सुनगुन बाहर खड़े व्यक्ति को शायद ही कभी मिल पाती हो। पता नहीं वह भीतर बैठा क्या करता रहता था ? कोई भी हो, क्या वह लम्बे वक्त तक महज दिवास्वप्नों में खोया रह सकता है ?
मैंने कुछ पलों के लिए अपने हाथ में लटका सूटकेस दहलीज पर टिका दिया था। जब भीतर से कोई आहट सुनाई नहीं पड़ी तो मैंने उसे उठाया और सोचा, फालतू में कयास लगाने में वक्त क्यों गँवाया जाए। कुछ खास तो वह कर नहीं रहा होगा-सीधे चलकर देख ही लिया जाए !
अभी चारेक दिन पहले मुझे उसका एक अन्तर्देशीय मिला था। वह चाहता तो दो-ढाई पंक्तियों के लिए एक कार्ड भी लिख सकता था। पर नहीं, फालतूपन से उसे कोई परहेज़ नहीं था। चींटे की टाँगों सरीखी लिखावट में उसने घसीट रखा था कि जरूरी सलाह-मशविरा करना है-इसे खास अहमियत दो।
मेरे पहुँचने पर जोर देने का यों कोई खास अर्थ नहीं था, क्योंकि मैं उसके स्वभाव से परिचित था। वह बहुत काहिल और आत्मकेन्द्रित व्यक्ति था। शायद सारी दुनिया में मैं ही एकमात्र वह शख़्श था जिसे वह भूले-भटके कभी पत्र लिखता होगा। उसका खत पाने के बाद मैं देर तक इस बात पर विचार करता रहता था कि उसने खत-लिफाफा या अन्तर्देशीय कैसे और कहाँ से प्राप्त किया होगा। वह तो अपने कोठड़े से निकलकर पोस्ट ऑफिस तक जाने से रहा। किसी ने खत लाकर दिया भी होगा तो कितने दिनों बाद उसे लिखने की नौबत आई होगी और फिर वह उसकी मेज पर इस प्रतीक्षा में बेचैन पड़ा रहा होगा कि उसकी उस जेलखाने से किसी प्रकार मुक्ति तो हो। उसके खत के सिरनामे पर कोई पता या तारीख अंकित नहीं होती थी। उसके खत बस इस बात के परिचायक होते थे कि वह किसी गहरे मानसिक द्वन्द्व से बाहर नहीं निकल पा रहा है।
उपरोक्त विवरण से आप यह न समझें कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात कह रहा हूँ जो मामूली पढ़ा-लिखा ऐसा अभिव्यक्ति विमुख जीव है जो लिखना-पढ़ना ही न जानता हो। वह उन्नीस सौ अड़तीस का सेन्ट जॉन्स कॉलेज का लॉ ग्रेजुएट था। पढ़ाई के बाद कुछ वर्ष यूरोप में भी घूम चुका था। मगर उसने कभी कोई काम हाथ में नहीं लिया था। यहाँ तक कि वकालत का लाइसेन्स लेने के बावजूद एक दिन के लिए भी किसी मुवक्किल के मुकद्दमे की पैरवी करने के लिए कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ था। हाँ, यह दीगर मुद्दा है कि परिवारी जमीन-जायदाद के मामले-मुकद्दमों में वह यदा-कदा कचहरी चला जाता था। जो उससे सलाह लेने आते थे उन्हें कानूनी दाँव-पेंच भी खूब समझा देता था।
उसका नाम कुँवर वीरेन्द्र बहादुर सिंह था। मगर मैं अथवा कोई पुराना दोस्त उसे सिर्फ कुँवर कहकर सम्बोधित करते थे। मैं अन्त तक उसका सहपाठी नहीं रह गया था। मैं मैट्रिक में उसके साथ था और बाद में वह बाहर पढ़ने चला गया था। हाई स्कूल में पढ़ते हुए भी वह फोर्ड गाड़ी में स्कूल आता था। यह उस दौर की बात है जब मेरे जैसे निम्न-मध्यवर्गीय परिवारों के विद्यार्थी पैदल चलकर ही स्कूल पहुँचते थे। बहुत हुआ तो कोई भाग्यशाली साइकिल पा जाता था। साइकिल की कीमत दस-पन्द्रह रुपये से अधिक नहीं थी, मगर वह-पन्द्रह भी किसको मयस्सर होते थे ?
मैंने दरवाज़े से चार-छह कदम आगे बढ़कर देखा कि कमर के पीछे दोनों हाथ बाँधे खोयेपन की मनःस्थिति में एक तख्त के इर्द-गिर्द चक्कर काट रहा है। जब मैंने पाया कि वह दरवाज़े से भीतर दाखिल होने वाले के अस्तित्व से पूरी तरह बेखबर है तो मैंनें आगे बढ़कर अपना सूटकेस तख्त पर टिका दिया।
मुझे अपने सामने देखकर वह ठहर तो गया पर उसके लम्बे-चौड़े मस्तक पर खिचीं अनगिनत रेखाएँ यथावत् बनी रहीं। आँखें उसी तरह चढ़ी हुई उसकी तुनकमिजाजी का हवाला देती रहीं। एक बहुत पुराना फौजी ओवरकोट उसकी तीन-चौथाई देहयष्टि को ढँके हुए था और कोट के कालर गर्दन को छिपाए हुए थे।
वह मुझसे कुछ नहीं बोला तो मैं आगे बढ़कर उसकी लम्बी-चौड़ी मसहरी की पाटी पर टिक गया। मैं उसकी इस तरह की कदीमी मनहूसियत से बाखबर था इसलिए मेज पर रखी सिगरेट की डिब्बी और लाइटर उठाकर सिगरेट जलाने में लग गया। उसने मुझे सिगरेट का लम्बा कश खींचते देखा और फिर चक्कर काटने लगा। मैंने जूते उतारे और पलँग पर पसर गया। उसके कमरे पर टीन की चादरें पड़ी थीं और सहन में खड़े नीम की पत्तियाँ टीन की छत पर गिरकर हल्की खड़क पैदा कर रही थीं।
मैंने स्वयं को हल्का छोड़ दिया और उसको उसके हाल पर चलने दिया। जब उसका जी भर जाएगा या चक्कर काटते-काटते पाँव थक जाएँगे तो वह स्वयं ही कुछ न कुछ बोलने लगेगा। ऐसे सिरफिरे आदमी को क्या कहा जाए जो अपने दोस्त को पत्र लिखकर तुरन्त चले आने का अनुरोध करता है और उसके आ जाने पर उससे फूटे मुँह कुछ बोलता-कहता तक नहीं है।
मैंने सिगरेट के कई लम्बे-लम्बे कश लिए और धुआँ ऊपर छत की ओर छोड़ते हुए करवट बदल ली और कुँअर के बारे में ही सोचने लगा।
कुँवर का पारिवारिक आवास एक किले सरीखा है जिसमें पैंतालीस-पचास छोटे बड़े कमरे, कोठरियाँ और दीवानखाने हैं। उस पूरी हवेली का एक बार जायजा लिया जाए तो दो घंटे से कम नहीं लगेंगे। दूर-दूर तक उस आवास को लाल हवेली के नाम से जाना और पुकारा जाता है। झिर्रियों और झिलमिली वाली खिड़कियों और दरवाजों से लैस तथा मेहराबों और कँगूरों से आवृत वह हवेली कम से कम दो सवा दो सौ साल पुरानी तो जरूर ही रही होगी। कस्बे के इस पुरातन भवन को भीतर से देखने की उत्कण्ठा कस्बे के बाशिन्दों की हसरत जैसी है। कुँअर ने उस हवेली के अन्तरंग से अपना सम्बन्ध बरसों पहले ही तोड़ लिया है और चहारदीवारी के अन्तिम छोर पर एक लम्बा-चौड़ा अनगढ़-सा कोठड़े बनवाकर पड़ा हुआ है। कोठड़े की बाजू में एक छोटी-सी कोठरी भी डलवा ली है जो मैंने पिछली बार नहीं देखी थी।
कस्बे की हवेली के अलावा बस्ती से कोई तीनेक मील के फासले पर सीकरी मौजे में भी एक किलानुमा गढ़ी है। वह तो शायद तीन सौ साल पुरानी होगी। कई एकड़ जमीन पर आबाद उस हवेली के सदर दरवाज़े के ऊपर जो मशाल जलती है उसे दूर-दूर तक के इलाके में देखा जाता है। पर ऐसे मौके अब गिने-चुने ही रह गए हैं, क्योंकि राजा हीरासिंह के देहावसान के बाद सीकरी में बरसों से कोई नहीं रहता। सौ-सवा सौ कमरों, बारादरियों, दीवानखानों वाली गढ़ी उपेक्षित पड़ी है। कुँवर वीरेन्द्रबहादुर के नाना राजा हीरासिंह कोठी के आखिरी उत्तराधिकारी थे। उन्होंने ही अपनी बड़ी बेटी और उसके बेटों को अपने संरक्षण में बुला लिया था और अपनी देख-रेख में उनकी परवरिश की थी। पूरे इलाके में राजा हीरासिंह का दबदबा था और आले दर्जे के हाकिम-हुक्काम आए दिन सीकरी में दिखाई पड़ते रहते थे। राजा साहब नाच-गाने और शिकार के जबरदस्त शौकीन थे। नाच-गानों के जश्न तो होते ही रहते थे-अंग्रेज अफसरों की अगवानी के अवसर पर तरह तरह के जश्न भी मनाए जाते थे। नौबतखाने में दस-बारह हाथी और घुड़साल में सौ-सवा सौ असली नस्ल के घोड़े खड़े हिनहिनाते रहते थे।
सीकरी के आसपास लगे सैकड़ों गाँवों में राजा हीरासिंह की रैयत फैली पड़ी थी। राजा हीरासिंह अपने पुरखों की ग्यारहवीं पीढ़ी के नौनिहाल थे। जिस समय उस गढ़ी का निर्माण हुआ था, अंग्रेजों के पाँव इस देश में पूरी तरह नहीं फैले थे। वह देशी राजे-रजवाड़ों का युग था और प्रत्येक प्रान्त में इस तरह के राव-राजे-सामन्त बिखरे पड़े थे। किसी को भी आज सीकरी के उस विशाल भवन को देखकर सहज ही आश्चर्य होगा, क्योंकि धुर देहात में उस तरह के निर्माण में जो श्रम और बुद्धि लगानी पड़ी होगी वह चकित करने वाली रही होगी।
जब मैं कुँवर के साथ पढ़ता था तो उसकी मेरे से अच्छी रब्त-जब्त हो गई थी। वह अपने वैभव में बेजोड़ था तो मैं अपने अभावों का जीता-जागता नमूना था। शायद वैभव भी कभी-कभी निर्धनता को देखकर चमत्कृत होता है और उसकी ओर हठात् खिंचता चला जाता है। कहाँ वह फोर्ड गाड़ी में ब्रीचेस और पम्पशू डाटकर आने वाला जैंटिलमैन और कहाँ मैं सूती कमीज और उठंग पाजामा पहनकर आने वाला निरीह-सा विद्यार्थी ! तीन या चार आने की जो सस्ती सी चप्पलें पहनकर मैं स्कूल पहुँचता था उन पर निगाह जाते ही मेरी विपन्नता का विराट स्वरूप सामने आ जाता था।
एक बार कुँवर मुझे बग्घी में अपने साथ बिठाकर सीकरी की उस आतंक जगाने वाली गढ़ी में ले गया था। मैं लम्बे-चौड़े रकबे में फैली उस इमारत में खो सा गया था। इधर-उधर घुमाने के बाद राजा हीरासिंह का दीवान मुझे एक बहुत बड़े हॉल में ले गया था। उस दीवानखाने की दीवारें बहुत ऊँची और छत झाड़-फानूसों से भरी हुई थी। मैंने सारी दीवारों पर हीरासिंह के वंश-वृक्ष की बड़ी-बड़ी आदमकद तस्वीरें स्वर्णाभ चौखटों में जड़ी देखी थीं। उन पुरखों की लम्बी-चौड़ी आकृतियाँ देखकर मन में सहसा एक विचित्र-सा आतंक पैदा हो जाता था।
गढ़ी नदी के बाएँ किनारे पर स्थिति थी। लम्बी-चौड़ी छतों से देखने पर नदी का महत्त्व और सुन्दरता समझ में आ जाती थी। यही-नहीं, उस विशाल गढ़ी में कई दीवानखाने थे। सभी बड़े कमरों की छतें भारी-भारी झाड़-फानूसों से सजी हुई थीं। छतों के कुंदों में कई स्थानों पर रंग-बिरंगे गोल-गोल हंडे भी लटके हुए थे। तरह-तरह की मूर्तियाँ और संगमरमर की छतरियाँ यहाँ-वहाँ देखी जा सकती थीं। लम्बे-चौड़े जलाशय और बागों में फव्वारे तो सब जगह नजर आते थे। पत्थरों के घाटों वाले सरोवर और स्फटिक-सा स्वच्छ उनमें भरा नीला जल मन को अनायस मोह लेता था।
यह सब भी तब तक बहुत पुराना हो चुका था। गढ़ी का वैभव और चहल-पहल राजा हीरासिंह के जीवित रहने की अवधि में ही निष्प्रभ होने लगी थी। मैं जब कई दशक पहले कुँवर के साथ वहाँ गया था तब तक कितने ही दास-दासियाँ वहाँ से विदा हो चुके थे और रनिवास भी सन्नाटे में डूबा हुआ था।
अब तो शायद बूढ़ा दीवान भी मर चुका था और सीकरी की हवेली पूरी तरह से निर्जन हो गई थी। वहाँ किसी के बने रहने की स्थितियाँ धीरे-धीरे दुर्वह होती चली गई थीं।
कुँवर के कस्बे से बाहर चले जाने पर मेरा उसके परिवार और सीकरी की गढ़ी से सम्बन्ध लगभग टूट ही गया था। कभी-कभी मैं कस्बे के बाजार में राजा हीरासिंह की गाड़ी खड़े देखता था। अंग्रेज बहादुर के रंग में रँग जाने के बाद उन्होंने अपने हाथी-घोड़े बेच दिए थे और अपनी फोर्ड पर ही शहर आते थे। उस गाड़ी को वह स्वयं ही चलाते थे। उनकी छत विहीन फोर्ड को हर कोई पहचानता था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह हाट-बाजार में चालू हालत में खड़ी रहती थी और उसके मडगार्ड बराबर हिलते रहते थे। कस्बे की लाल हवेली के बाहर तो वह गाड़ी अक्सर खड़ी ही रहती थी।
राजा हीरासिंह की देह गुलाबी गोरापन लिए हुए थी और उनकी आँखें नीले काँच की गोलियों सरीखी नज़र आती थीं। उनके सिर पर खाकी रंग का हैट होता था। खाकी बिरजेस और खुले कालर वाले कोट में वह अपने रूप-रंग से बजाय राजा के किसी अंग्रेज सार्जेण्ट जैसे दीख पड़ते थे।
बुढ़ापे के दिनों में राजा हीरासिंह के हाथ-पैर ही क्या बल्कि सारा शरीर ही हिलने लगा था। मैंने उन्हें कितनी ही दफा बीच सड़क में मोटर रोककर कस्बे के लोगों से बतियाते देखा था। राजा का खिताब पाने के बाद भी उनमें कोई राजसी ठसक दिखाई नहीं पड़ती थी। वह जनसाधारण से भी एक सहज-सरल बुजुर्ग की तरह पेश आते थे। इधर उनके हाथ और सिर हिलता रहता था उधर-मोटर के इंजन के चालू होने की वजह से उसकी भी बाँडी काँपती-काँखती रहती थी। मोटर और उनकी स्थिति समान हो चली थी-गोया मोटर भी उनकी तरह की पार किन्सन रोग से ग्रस्त हो गई थी।
राजा हीरासिंह की पाटदार आवाज़ में भी कंप का स्पष्ट आभास मिलता था। बहुत बाद में जब बोलती फिल्में हमारे कस्बे के सिनेमाहॉल में दिखाई जाने लगीं तो मैंने राजा हीरासिंह की शक्ल-सूरत से मिलता-जुलता एक अभिनेता देखा था। बाद में पता चला कि उसका नाम चन्द्रमोहन था।
लोगों का खयाल था कि राजा हीरासिंह अचूक निशानेबाज थे। बुढ़ौती में भी वह अंग्रेजों और देशी हुक्कामों के साथ खूब सैर-सपाटों पर जाते थे और शिकार में तो खास तौर से सम्मिलित रहते थे। यह कभी नहीं हुआ कि उनकी बन्दूक की नली से निकली गोली व्यर्थ गई हो।
राजा हीरासिंह जी की मौज-मस्ती, ऐश और अय्याशी में तीन-चौथाई जायदाद तो उनके सामने ही बिक चुकी थी। जो रेहन रखी गई थी वह भी कभी नहीं छुड़ाई जा सकी। पर एक बात ऐसी थी कि जिसमें कभी कोताही नहीं हुई-राजा साहब अधिक-से-अधिक समय अपनी सीकरी की गढ़ी में ही बिताते थे। कुँवर वीरेन्द्रबहादुर सिंह और उनके बड़े-भाई कुँवर रामपाल सिंह का परिवार भी यदा-कदा सीकरी जाता रहता था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कुँवर लोगों तथा उनके परिवारों का सीकरी जाना तभी तक सम्भव हो पाया जब तक राजा हीरासिंह जीवित रहे। चूँकि उनकी पत्नी का देहान्त चालीस-पैंतालीस की उम्र में ही हो चुका था और उनकी एकमात्र सन्तान वह बेटी ही थी जिसके बेटे कुँवर बीरेन्द्रबहादुर और कुँवर रामपाल सिंह थे। इसलिए बाद में गढ़ी एक तरह से खाली ही पड़ी रह गई। शहर या कस्बे की कोई इमारत होती तो उसकी अच्छी कीमत लग जाती, मगर गाँव में उस महल को कोई क्यों खरीदता ? बस बाद में एक-दो नौकर-चाकर या पुराने कारिन्दे ही उसमें रहते रहे।
मैं पुरानी यादों में डूबा हुआ था और यह बिल्कुल भूल चुका था कि मैं कुँवर बीरेन्द्रबहादुर के कोठड़े में उनके पलँग पर पड़ा दिवास्वप्न ले रहा हूँ। तभी कोई धम्म से टीन की छत पर कूदा। इसके कई मिनट बाद तक धम-धम की आवाजें होती रहीं तो मैं पलँग से उठा और सामने वाले दरवाज़े से बाहर निकल गया। बन्दरों की पूरी फौज नीम के पेड़ से कूद-कूदकर छत पर इकट्ठी हो गई थी।
मैं कमरे में वापस लौटा तो मैंने कुँवर को बदस्तूर चक्कर काटते देखकर मुस्कराते हुआ कहा, ‘‘कुँवर बहादुर को लंका जीतने का न्यौता देने के लिए पूरी वानर सेना छत पर सजी बैठी है।’’
कुँवर मेरा व्यंग्य सुनकर ठहर गया और आँखें माथे पर चढ़ा लीं। उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला-जैसे वह एकदम गूँगा-बहरा हो गया। पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा था कि वह अजीब-खब्ती जैसा होता चला जा रहा था। हँसना किस चिड़िया का नाम होता है यह तो वह जैसे भूल की चुका था। मैंने दिमाग पर जोर देकर बहुत सोचा कि मैंने उसे पिछली बार हँसते या मुस्कराते कब देखा था-पर मुझे वह अवसर याद नहीं आया। घर-परिवार को लेकर उसे कितनी गहरी विरक्ति हो चली थी इसका अनुमान तो बस इसी बात से लगाया जा सकता था कि वह चहारदीवारी में ही खड़ी हवेली की ओर कभी झाँकता भी नहीं था। एक नौकर इस टीन शेड में दोनों समय का खाना पहुँचा जाता था। उसकी जिन्दगी का एक दिन नज़दीक से देख लेने मात्र से उसकी जीवनचर्या को बखूबी समझा जा सकता था। वह एक अजीब मनहूस और अजनबियत-भरी जिन्दगी जी रहा था-जिसे सन्दर्भों से कटी हुई और पूरी तरह अप्रासंगिक कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं मानी जानी चाहिए।
आपने ऐसी कोई नीरस कहानी अवश्य पढ़ी या सुनी होगी जिसमें महज एक आदमी होता है जो कमरे में बैठा या इधर-उधर टहलता रहता है। सिगरेट के बाद सिगरेट फूँकता चला जाता है। इसके अलावा वहाँ कुछ भी उल्लेखनीय घटित नहीं होता। कमरा धुएँ के घोट से घुटता रहता है और वह मनहूस आदमी उसमें घुटकर खाँसता या काँखता रहता है। शायद आपने ऐसी कहानी न भी पढ़ी या सुनी हो, मगर यह इस जीवन और दुनिया की एक त्रासद सच्चाई है कि ऐसा होता है और इस पृथ्वीतल पर ऐसे न जाने कितने पात्र हैं जो व्यर्थता की भूमिकाओं में साँस ले रहे हैं। जब भी मैं कुँअर को देखता था मुझे उपरोक्त नीरस कहानी एकदम सच्ची और अपने सामने घटित होती दिखाई पड़ने लगती थी।
अपने परिचय और अन्तरंग दायरे में मैंने कुँअर जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं देखा। सुबह उठकर बिजली के चूल्हे पर वह अपनी चाय खुद तैयार करता था। चूँकि उसका कोठड़ा पिछले गेट के नजदीक पड़ता था, इसलिए वह दरवाज़े के सामने की गली से गुजरने वाले किसी भी आदमी या लड़के-बाले को पकड़ बुलाता और अपनी आवश्यकता का सामान उससे मँगवा लेता था। सारा कस्बा राजा हीरासिंह के धेवतों के रौब-दाब से परिचित था, इसलिए उस परिवार के छोटे-मोटे कामों को पूरा करने के लिए हर कोई खुशी से तैयार हो जाता था। सामन्ती दबदबा तो उस वक्त तक इस कदर दम तोड़ चुका था कि किले सरीखी लाल हवेली की बरसों तक सफाई-पुताई भी सम्भव नहीं हो पाती थी। लम्बे समय की अय्याशी, काहिली और परोपजीवी बने रहने की मानसिकता ने सबको आरामतलबी और जड़ता की जंजीरों में जकड़कर रख दिया था। बड़े कुँवर रामपाल सिंह न जाने कितनी कम्पनियों के मैनेजिंग डॉयरेक्टर के साथ-साथ और भी न जाने क्या-क्या थे। मगर अपनी सामन्ती ठसक में कहीं से कुछ कमाने के बजाय बड़े आदमियों को अपनी हवेली में पार्टियाँ देने के चक्कर में अपनी गाँठ का ही बहुत कुछ गँवा देते थे। लगता था जैसे वह सहज अपने बड़प्पन को बनाए रखने के उद्देश्य से ही सभा-सम्मेलनों और कम्पनियों से जुड़े रहते थे।
दोनों कुँवरों के बेटे-बेटियाँ बाहर के बड़े शहरों में हॉस्टलों में रहकर महँगी पढ़ाई कर रहे थे। कुँवर वीरेन्द्र सिंह का बड़ा बेटा रेलवे इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी करके कलकत्ता में अप्रेन्टिसशिप का कार्यकाल पूरा कर रहा था और कुँवर रामपाल सिंह का बेटा इंजीनियर्स इंडिया में कार्यरत था। इन दोनों लड़कों में से कभी कोई अपनी जन्मभूमि यानी उनींदे कस्बे में आना तथा लाल हवेली में रहना गवारा नहीं करता था। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी दरबारी संस्कृति के प्रति उन्हें किसी प्रकार का लगाव नहीं था, बल्कि यह कहना ज्यादा सच होगा कि उन्हें सामन्ती रखरखाव के प्रति घोर वितृष्णा थी।
कुँवर परिवार के पास कितने ही गाँवों की सम्पत्ति थी पर उन्होंने जमीन को कभी हाथ नहीं लगाया था। खुद काश्त न होने की वजह से लगभग सारा इलाका उनके हाथ से निकल चुका था। जमींदारी की सम्पत्ति की घोषणा के बाद उन्हें जो भी मुआवज़ा मिलता था वह ऊँट के मुँह में जीरा की कहावत को अक्षरशः चरितार्थ करता था। अभी भी कस्बे की पुरानी जायदादें बेचकर ही रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की जा रही थीं। कभी-कभी तो यह तक भी होता था कि घर का कोई पुराना खैरख्वाह चुपके से हवेली में बुलाया जाता था और बड़ी कुँवरानी (कुँवरों की माँ हीराबेन) कोई जेवर या जवाहरात उसको सौंपकर किसी दूसरे शहर में बिकवाती थी और इस प्रकार घर-परिवार की ठप्प होती गति को संचालित करती थी।
मैं जब पिछली बार हवेली में आया था तो मुझे कुँवर रामपाल सिंह ने बतलाया था कि कुँवर वीरेन्द्र सिंह अपने हिस्से का मुआवजा खुद ही वसूल करता था। उसने पूरे परिवार की बिगड़ती स्थिति की ओर से पूरी तरह आँखें मूँद ली थीं। दिन छुपते ही शराब की पूरी भरी बोतल लेकर बैठ जाता था। जब बोतल खत्म हो जाती थी तो सदर दरवाज़े पर जाकर खड़ा हो जाता था और नशे की हालत में सड़क से गुजरते किसी को भी बुलाकर देसी शराब के ठेके से सस्ती शराब की बोतल मँगवा लेता था।
कुँवर रामपाल सिंह के कथन की सच्चाई मैंने कुँवर वीरेन्द्र सिंह के कमरे में घुसते ही भाँप ली थी। उसके पलँग के नीचे अंग्रेजी और देसी शराब की खाली बोतलों का अंबार लगा हुआ था।
बहुत पहले जब कुँवर ने कानून की पढ़ाई पूरी की थी तो उसकी सेहत देखने के काबिल थी। उसके कद्दावर और संतुलित शरीर को देखकर किसी को भी ईर्ष्या हो सकती थी। पर अब उसे देखकर तरस आता था। उसका चेहरा काला पड़ गया था। स्वास्थ्य इसी सीमा तक चौपट हो चुका था कि वह महज एक लम्बा-चौड़ा ढाँचा भर रह गया था।
उससे लम्बे समय की यारी-दोस्ती थी इसलिए मेरा उसके पास पहुँचना किसी समय-विशेष का मोहताज नहीं था; बाकी तो दिन छिपने के बाद उसे अपने कमरे की दहलीज पार करने वाले पर इतना गुस्सा आता था कि वह कुछ भी कर सकता था। किसी तरह हम दोनों की राह-रस्म बस निभती ही चली आ रही थी, क्योंकि सारा लोक-व्यवहार लँगड़ा और पूरी तरह इकतरफा था। वह स्वयं तो इस सीमा तक आत्मकेन्द्रित था कि किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता था। वह बहुत कुछ पशु-प्रवृत्ति से ग्रस्त हो चला था।
अक्सर तो उसके कोठड़े के दरवाज़े साँझ होते ही बन्द हो जाते थे। कोई भूले-भटके उसके दरवाज़े पर दस्तक दे भी देता तो वह कड़ककर पूछता, ‘कौन ?’ यही नहीं ‘कौन’ बोलने के साथ ही वह पलँग पर पड़ी भरी बंदूक उठाकर खड़ा हो जाता था। उसके इस प्रकार के आवेश-भरे व्यवहार पर कभी-कभी मैं हँस भी पड़ता था। मेरे चेहरे पर हँसी देखकर वह अपने होंठ चबाने लगता था। एक बार तो टिन शेड की बगल में खड़े लहीम-शहीम नीम के पेड़ पर कुछ हलचल की आहट पाते ही उसने बाहर जाकर बन्दूक दाग दी। बाद में पाया गया कि कोई भी हादसा नहीं गुजरा। नीम पर बैठा एक बन्दर धाँय की आवाज़ से डरकर टिन पर गिर पड़ा और साथ ही नीम की एक बड़ी-सी शाख टूटकर टिन की छत पर आ गिरी। संयोग से इस हास्यास्पद घटना के समय मैं उसके कोठड़े में मौजूद था। मगर मेरे ठठाकर हँसने के बावजूद उस पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। वह नशे में गलतान था और चेहरा तना, आँखें हमेशा की तरह कपाल पर चढ़ी हुई थीं। उसके भीतर जो बेचैनी का तूफान उमड़ता रहता था उसे वह कोठड़े में चक्कर काटकर ही सहन करता था। उसे यों घूमते, चक्कर काटते देखकर यही अहसास होता था जैसे कोई घायल पशु तकलीफज़दा हालत में अपने बाड़े में घूम-फिर रहा हो।
ऐसा भी कई बार होता था कि मैं उसके पास पहुँचने के अवसर टालता चला जाता था। ऐसी स्थिति में मुझे उसका तार मिलता था : समथिंग इम्पार्टेण्ट टु बी डिसकस्ड (आवश्यक मुद्दे पर विचार-विमर्श)।
अगर मैं तार की भी परवाह नहीं करता था तो वह मुझे नाराज़ खयाल करता था और बैरंग खत भेज देता था। जब उसके पास पहुँचता था, प्रायः शाम या रात हो जाती थी। अपनी पूरी सख्ती और तने हुए चेहरे के बावजूद वह मुझे बहुत निरीह, दयनीय और टूटा हुआ नज़र आता था। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती थी तो मैं नाराज होकर कहता था, ‘कुँवर, उस जहर पर काबू करो, ये तुम्हें ले बैठेगा। क्या हिकारत के अलावा तुम्हारी जिन्दगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है ?’
मुझे खुश करने की नीयत से वह दोनों कानों पर हाथ रखकर आगे कभी न पीने की तौबा करता था-शराब को भद्दी-भद्दी गालियाँ देता था। उसकी इस हरकत पर मुझे हँसी आने लगती थी। मैं उसकी भावुकता और ऐसे हवाई वायदों को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। यह बात मुझसे छिपी नहीं थी कि यह सब रात-भर का कौल करार है, दिन निकलते ही उसकी सारी विनम्रता और भावुकता हवा हो जाएगी। वह हमेशा की तरह वही पुराना कुँवर-सागर-तट पर फैली बालू जैसा शुष्क और किरकिरा हो उठेगा।
मैंने पिछली घटनाओं से उबरते हुए सिगरेट की डिब्बी से एक सिगरेट खींची और लाइटर से जलाकर नाक और मुँह से खिलन्दड़ेपन से धुआँ छोड़ने लगा।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i