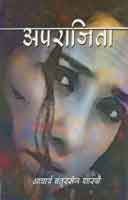|
नारी विमर्श >> अपराजिता अपराजिताआचार्य चतुरसेन
|
146 पाठक हैं |
|||||||
नारी समस्या पर आधारित एक रोचक उपन्यास.
उत्तप्त जल-कण
जब से प्रैक्टिस छोड़ी और कलम-घिसाई का धन्धा
अख्तियार
किया, तंगदस्ती बढ़ती ही गई। अजब नहीं, एक दिन भूखों मरने की नौबत आ जाए।
परन्तु मुझ ‘इच्छा-दरिद्री’ को इसकी शिकायत क्या ?
महीनों से बच्चे फटे हाल स्कूल जा रहे थे। उस दिन बाजार में कपड़े का एक पीस सस्ता मिल गया। इत्तफाक से पैसे जेब में थे—खरीद लाया। घर आकर प्रभा से कहा—‘‘इस कपड़े का तू फ्रॉक बनवाएगी या प्रकाश का बुश-शर्ट बनवा दूँ ?’’ उसने कोमलता से हँसकर कहा—‘‘प्रकाश का बुश-शर्ट बनवा दीजिए।’’ और चली गई। फिर मैंने प्रकाश को बुलाकर पूछा—‘‘इस कपड़े का तू बुश-शर्ट बनवाएगा या मैं प्रभा का फ्रॉक बनवा दूँ।’’ उसने झटककर कपड़ा मेरे हाथ से खींच लिया और उसे लेकर हँसता और यह कहता हुआ भाग गया—‘‘मैं बुश-शर्ट बनवाऊँगा।’’
साहित्यकार खब्ती तो होते ही हैं। बहुत देर तक मैं इस अत्यन्त छोटी-सी बात पर विचार करता रहा। विचार करते-करते बहुत पुरानी—साठ वर्ष पहली धुँधली स्मृतियाँ मानस-पटल पर उदित हो आईं। पिताजी कभी नाराज होकर मुझे एकआध चपत मार देते थे या गुस्सा होकर बकते थे तो कला की आँखों में पानी भर आता था। कला मुझसे बहुत छोटी थी—नासमझ थी—फिर भी जो चपत मुझ पर पड़ती थी, उसकी चोट न जाने कहाँ-कैसे उसे लग जाती थी, क्यों उसकी आँखें भर आती थीं, तब मैंने यह मर्म नहीं समझा था, इस पर विचार भी नहीं किया था। परन्तु इसके बाद ही नारी-जाति से मेरा परिचय बढ़ता ही गया। बचपन में मैंने अपनी माता की निरीह असहाय अवस्था देखी, अपने परिजन, पास-पड़ोस की स्त्रियों की दुरावस्था को देखा, कोई पति से पिटती थी और रोती हुई माता के पास आकर फरियाद करती थी, कोई आधी रात से सूर्योदय तक चक्की पीसकर अपना और बच्चों का पेट पालती थी। कोई बालिका विधवा, कोई युवती पति से त्यागी जाकर पिता के घर-भर के तिरस्कार सह रही थी। एक बार अपने पड़ोस की एक सात वर्ष की बालिका को, जब मैंने इसलिए फूट-फूटकर रोते देखा कि उसकी माता ने उसकी एक ही दिन पहले पहनी चूड़ियों को पत्थर से चकनाचूर कर दिया, क्योंकि उसके विधवा होने का तार ससुराल से आया था। वह सिसक-सिसककर रो रही थी। विधवा होने के कारण नहीं—चार पैसे की चूड़ियों के कारण !!!
मेरी आँखें खुलती गईं, और नारी की भावुकता और पीड़ा मेरे अंग में प्रवेश करती गई। तब से अब तक, बहुत बार मुझे उनके लिए आँखों का पानी बहाना पड़ा। और एक दिन एक असहाय नव-प्रसूता को एक तनिक से अपराध में जब उसके पति ने निर्दय होकर खूब पीटा, उसके सब जेवर उतार लिए, उसे जाड़ों की सूनी, काली और ठण्डी रात में धक्का देकर घर से निकाल घर में ताला बन्द कर दिया। बेचारी असहाय नारी—अस्मत, गैरत, लाज और मर्यादा से लदी-फदी किसी पास-पड़ोसिन के यहाँ शरण न जा सकी—अफीम निगल गई। भोर के तड़के मैं उधर होकर शौच के लिए निकला—अँधेरे में ठोकर लगी। अरे, यह राह में कौन सो रहा है ? देखा तो, की बहू ! आँखें पथराईं, मुँह से फेन निकलता हुआ—बदन ठ़ण्डा बर्फ लकड़ी-सा ऐंठा हुआ, छाती पर सूखे स्तन चूसती हुई नवजात बालिका। हे राम, हे राम ! मैं दौड़ा-दौड़ा माता के पास गया। माँ ने उठाकर उसे बिछौने पर सुलाया—उपचार किया। माँ को उसने धन्यवाद नहीं दिया, आँखों में पानी भरकर कहा—‘‘अम्मा, अच्छा नहीं किया, मुझे दुःख-सागर में फिर धकेल लाईं, मैं जा रही थी सुख-सागर में गोते लगाने।’’ और माँ ने अपनी चिरअभ्यस्त गाली दी—‘‘पगली, ले दूध पी !’’ और गर्म दूध का गिलास उसके सूखे-शीतल होंठों से लगा दिया। तीन दिन मैं उस नारी की खाट के पास पाटी पर सिर टेके बैठा रहा। सेवा-टहल कुछ नहीं की, सिर्फ कभी-कभी पूछता—‘‘अब कैसी हो भाभी, क्या अम्मा को बुलाऊँ ?’’ और उसका जवाब था—‘‘नहीं भैया, मैं अच्छी हूँ।’’ इसके बाद पानी-पानी-पानी। वही आँखों का पानी।
इससे तो मेरी आँखों का पानी झुसल उठा। वह उत्तप्त होकर चार-चार धार बहने लगा। कितना बहा—अब इसका हिसाब-किताब क्या दूँ ? एक-दो दिन का खाता नहीं है, साठ साल से कुछ ऊपर ही का जमा-खर्च है।
इस बीच—ज्ञान, विज्ञान, धर्म, नीति, समाज-राजनीति और अर्थशास्त्र के गहन वनों में होकर जीवन पार करना पड़ा, सम्पत्ति और विपत्तियों ने प्राणों को बहुत झकझोरा, बहुत बार जीवन-मरण की समस्याएँ आईं, अनगिनत शत्रु और मित्रों से हाथ मिले, आँखें मिलीं, परन्तु वह ‘नारी’ जो हृदय में बैठी-सो-बैठी, आँसू से भरी हुई, दर्द से कराहती हुई, निराशा से लाचार, असहाय बेबस।
चार युग देखते-ही-देखते ही बीत गए। युग ने पलटा खाया, नारी की दर्दभरी कराह-क्रोध की चीत्कार और आवेश फूत्कार में बदल गई। मेरी माँ, दादी, चाची, भाभियों और बहनों की छाया कभी भी दहलीज के बाहर नहीं हुई। लक्ष्मण की खींची हुई रेखा को जैसे रावण को भिक्षा देने आकर सीता के उल्लंघन करने में आपत्ति थी, वैसे ही अपने छकड़ा भरे दुख-सुख को लेकर घर की दहलीज से बाहर निकलना उनकी मर्यादा से बाहर था। घर ही में वे जन्मीं, बढ़ीं, जीईं, और मरीं। परन्तु आज की मेरी बेटियों ने उस लक्ष्मण की रेखा का—घर की दहलीज का—उल्लंघन कर दिया, उन्होंने कालेज से उच्च शिक्षाएँ प्राप्त की हैं, वे जीवन के संघर्ष में पुरुषों की प्रतिस्पर्द्धा करने लगी हैं। साहस और प्रतिभा का जहाँ तक सवाल है, वे पुरुषों से आगे हैं। पाश्चात्यों के संग ने हमारी नारी-समस्या को भारी उलझन में डाल दिया है और आज केवल हमारा ही नहीं—सारे ही संसार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रश्न—यह उठ खड़ा हुआ है कि ‘‘नारी का समाज में क्या स्थान होगा ?’’ सभ्य संसार के सामने बड़े-बड़े विकट राजनैतिक और आर्थिक प्रश्न हैं, परन्तु मेरा ख्याल है कि दुनिया के मेधावी उन प्रश्नों का हल निकाल लेंगे, परन्तु इस नारी-समस्या का नहीं।
सभ्य-शिष्ट-समुन्नत नारी-समाज ने घर की दहलीज का उल्लंघन अवश्य किया है, पर ऐसा करके उसने रावण के द्वारा हरण किए जाने ही का खतरा उठाया है। ‘पुरुष’ यह छद्मवेशी राक्षस—साधु के वेश में भिक्षा के मिस उसे हरण करने की ताक में है। नारी को—उसके साहस ने, शिक्षा ने, समुन्नत होने से तनिक भी तो सहारा नहीं दिया है। बन्धुवर मैथिलीशरण गुप्त ने तो एक ही वाक्य में नारी का सब-कुछ बखान कर दिया—‘‘आँचल में है दूध, और आँखों में पानी।’’ अब वह नारी धन-दौलत, शिक्षा और सारी विभूतियों से लदी-फदी रहे, उसका सच्चा परिचय तो यही है—‘‘आँचल में है दूध और आँखों में पानी।’’
मैं तो पहले ही कह चुका हूँ—इस पानी में मैंने भी अपनी आँख का बहुत पानी मिलाया है, अलबत्ता, इसका कोई साक्षी नहीं है, परन्तु यह दूध का ऋण नहीं है, यह तो मेरे ‘जीवन’ का ऋण है। मैं तो यही समझता हूँ, और क्या समझते हैं—मैं नहीं जानता।
मैं चिकित्सक भी तो हूँ। और पचास वर्षों के अनुभव से मैंने एक चिकित्सा-तत्त्व पाया है, ‘विषस्य विषमौषधम्।’ यह बड़ा भारी गूढ़ तत्त्व है।
इसी तत्त्व पर मैंने ‘नारी-समस्या’ को भी परखा है। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच हूँ कि नारी ही नारी की समस्या को हल कर सकती है, परन्तु ‘नारी’ रहकर। ‘नर बनकर नहीं।’ ‘नारी’ बनने के लिए उसे ‘नारी-तत्त्व’ को जीवन में आत्मसात् करना होगा। ऐसा करने ही से वह, ‘अपराजिता’ के रूप में उदय होगी।
बीस बरस से मैं इस ‘अपराजिता’ नारी की खोज में था—कहीं मिलती ही न थी। इस बार जुलाई मास में बनारस गया। सख्त गर्मी थी, पंखा पास न था। बिस्तर भी नाकाफी था। मस्तिष्क में अनेक उलझनें भरी हुई थीं। वर्षा नहीं हो रही थी, हवा नहीं चल रही थी। खुली छत सोने के लिए नहीं थी। सब जड़-जंगम सरंजाम ऐसे जुट गए थे कि ‘निन्दिया रानी’ आई ही नहीं। अकस्मात् उस अर्ध निशा में ‘राज’ से साक्षात् हुआ। ‘ब्रज’ और ‘राधा’ उसी के साथ थे। तीनों बातें करने लगे। तीनों नहीं दोनों—‘राज’ और ‘राधा’। ब्रज सुनता था, केवल हँसता था। मैं भी सुनने लगा। सब बातें पते की थीं। कलम मेरे पास थी—और कागज भी। जो कुछ सुना, लिख डाला। और तब मैंने देखा—ओह, यह ‘राज’ तो सारे संसार की सभ्य-असभ्य नारियों से पृथक् अकेली ही खड़ी है। केवल अपनी ही सामर्थ्य पर। वह असहाय नहीं है, परमुखापेक्षी नहीं है—क्रोध, दैन्य, आवेश अधैर्य, सबसे पाक-साफ है। वह संयम-कर्तव्य और जीवन के सच्चे तत्त्वों की अधिष्ठात्री है। वह आज की नारी-मात्र की पथ-प्रदर्शिका है। मैंने उसे अपराजिता स्वीकार कर लिया। और उस दिन ‘ब्रजराज’ ने राज के चले जाने के बाद—जब उस भूमि पर—जहाँ उसके चरण-चिह्न बने थे—साष्टांग भू-पात करके अपना मस्तक टेक दिया—तो सबकी नजर बचाकर मैंने भी उन चरण-चिह्नों की एक कोर चूम ली। और मेरा अब तक का जीवन धन्य हो गया।
महीनों से बच्चे फटे हाल स्कूल जा रहे थे। उस दिन बाजार में कपड़े का एक पीस सस्ता मिल गया। इत्तफाक से पैसे जेब में थे—खरीद लाया। घर आकर प्रभा से कहा—‘‘इस कपड़े का तू फ्रॉक बनवाएगी या प्रकाश का बुश-शर्ट बनवा दूँ ?’’ उसने कोमलता से हँसकर कहा—‘‘प्रकाश का बुश-शर्ट बनवा दीजिए।’’ और चली गई। फिर मैंने प्रकाश को बुलाकर पूछा—‘‘इस कपड़े का तू बुश-शर्ट बनवाएगा या मैं प्रभा का फ्रॉक बनवा दूँ।’’ उसने झटककर कपड़ा मेरे हाथ से खींच लिया और उसे लेकर हँसता और यह कहता हुआ भाग गया—‘‘मैं बुश-शर्ट बनवाऊँगा।’’
साहित्यकार खब्ती तो होते ही हैं। बहुत देर तक मैं इस अत्यन्त छोटी-सी बात पर विचार करता रहा। विचार करते-करते बहुत पुरानी—साठ वर्ष पहली धुँधली स्मृतियाँ मानस-पटल पर उदित हो आईं। पिताजी कभी नाराज होकर मुझे एकआध चपत मार देते थे या गुस्सा होकर बकते थे तो कला की आँखों में पानी भर आता था। कला मुझसे बहुत छोटी थी—नासमझ थी—फिर भी जो चपत मुझ पर पड़ती थी, उसकी चोट न जाने कहाँ-कैसे उसे लग जाती थी, क्यों उसकी आँखें भर आती थीं, तब मैंने यह मर्म नहीं समझा था, इस पर विचार भी नहीं किया था। परन्तु इसके बाद ही नारी-जाति से मेरा परिचय बढ़ता ही गया। बचपन में मैंने अपनी माता की निरीह असहाय अवस्था देखी, अपने परिजन, पास-पड़ोस की स्त्रियों की दुरावस्था को देखा, कोई पति से पिटती थी और रोती हुई माता के पास आकर फरियाद करती थी, कोई आधी रात से सूर्योदय तक चक्की पीसकर अपना और बच्चों का पेट पालती थी। कोई बालिका विधवा, कोई युवती पति से त्यागी जाकर पिता के घर-भर के तिरस्कार सह रही थी। एक बार अपने पड़ोस की एक सात वर्ष की बालिका को, जब मैंने इसलिए फूट-फूटकर रोते देखा कि उसकी माता ने उसकी एक ही दिन पहले पहनी चूड़ियों को पत्थर से चकनाचूर कर दिया, क्योंकि उसके विधवा होने का तार ससुराल से आया था। वह सिसक-सिसककर रो रही थी। विधवा होने के कारण नहीं—चार पैसे की चूड़ियों के कारण !!!
मेरी आँखें खुलती गईं, और नारी की भावुकता और पीड़ा मेरे अंग में प्रवेश करती गई। तब से अब तक, बहुत बार मुझे उनके लिए आँखों का पानी बहाना पड़ा। और एक दिन एक असहाय नव-प्रसूता को एक तनिक से अपराध में जब उसके पति ने निर्दय होकर खूब पीटा, उसके सब जेवर उतार लिए, उसे जाड़ों की सूनी, काली और ठण्डी रात में धक्का देकर घर से निकाल घर में ताला बन्द कर दिया। बेचारी असहाय नारी—अस्मत, गैरत, लाज और मर्यादा से लदी-फदी किसी पास-पड़ोसिन के यहाँ शरण न जा सकी—अफीम निगल गई। भोर के तड़के मैं उधर होकर शौच के लिए निकला—अँधेरे में ठोकर लगी। अरे, यह राह में कौन सो रहा है ? देखा तो, की बहू ! आँखें पथराईं, मुँह से फेन निकलता हुआ—बदन ठ़ण्डा बर्फ लकड़ी-सा ऐंठा हुआ, छाती पर सूखे स्तन चूसती हुई नवजात बालिका। हे राम, हे राम ! मैं दौड़ा-दौड़ा माता के पास गया। माँ ने उठाकर उसे बिछौने पर सुलाया—उपचार किया। माँ को उसने धन्यवाद नहीं दिया, आँखों में पानी भरकर कहा—‘‘अम्मा, अच्छा नहीं किया, मुझे दुःख-सागर में फिर धकेल लाईं, मैं जा रही थी सुख-सागर में गोते लगाने।’’ और माँ ने अपनी चिरअभ्यस्त गाली दी—‘‘पगली, ले दूध पी !’’ और गर्म दूध का गिलास उसके सूखे-शीतल होंठों से लगा दिया। तीन दिन मैं उस नारी की खाट के पास पाटी पर सिर टेके बैठा रहा। सेवा-टहल कुछ नहीं की, सिर्फ कभी-कभी पूछता—‘‘अब कैसी हो भाभी, क्या अम्मा को बुलाऊँ ?’’ और उसका जवाब था—‘‘नहीं भैया, मैं अच्छी हूँ।’’ इसके बाद पानी-पानी-पानी। वही आँखों का पानी।
इससे तो मेरी आँखों का पानी झुसल उठा। वह उत्तप्त होकर चार-चार धार बहने लगा। कितना बहा—अब इसका हिसाब-किताब क्या दूँ ? एक-दो दिन का खाता नहीं है, साठ साल से कुछ ऊपर ही का जमा-खर्च है।
इस बीच—ज्ञान, विज्ञान, धर्म, नीति, समाज-राजनीति और अर्थशास्त्र के गहन वनों में होकर जीवन पार करना पड़ा, सम्पत्ति और विपत्तियों ने प्राणों को बहुत झकझोरा, बहुत बार जीवन-मरण की समस्याएँ आईं, अनगिनत शत्रु और मित्रों से हाथ मिले, आँखें मिलीं, परन्तु वह ‘नारी’ जो हृदय में बैठी-सो-बैठी, आँसू से भरी हुई, दर्द से कराहती हुई, निराशा से लाचार, असहाय बेबस।
चार युग देखते-ही-देखते ही बीत गए। युग ने पलटा खाया, नारी की दर्दभरी कराह-क्रोध की चीत्कार और आवेश फूत्कार में बदल गई। मेरी माँ, दादी, चाची, भाभियों और बहनों की छाया कभी भी दहलीज के बाहर नहीं हुई। लक्ष्मण की खींची हुई रेखा को जैसे रावण को भिक्षा देने आकर सीता के उल्लंघन करने में आपत्ति थी, वैसे ही अपने छकड़ा भरे दुख-सुख को लेकर घर की दहलीज से बाहर निकलना उनकी मर्यादा से बाहर था। घर ही में वे जन्मीं, बढ़ीं, जीईं, और मरीं। परन्तु आज की मेरी बेटियों ने उस लक्ष्मण की रेखा का—घर की दहलीज का—उल्लंघन कर दिया, उन्होंने कालेज से उच्च शिक्षाएँ प्राप्त की हैं, वे जीवन के संघर्ष में पुरुषों की प्रतिस्पर्द्धा करने लगी हैं। साहस और प्रतिभा का जहाँ तक सवाल है, वे पुरुषों से आगे हैं। पाश्चात्यों के संग ने हमारी नारी-समस्या को भारी उलझन में डाल दिया है और आज केवल हमारा ही नहीं—सारे ही संसार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रश्न—यह उठ खड़ा हुआ है कि ‘‘नारी का समाज में क्या स्थान होगा ?’’ सभ्य संसार के सामने बड़े-बड़े विकट राजनैतिक और आर्थिक प्रश्न हैं, परन्तु मेरा ख्याल है कि दुनिया के मेधावी उन प्रश्नों का हल निकाल लेंगे, परन्तु इस नारी-समस्या का नहीं।
सभ्य-शिष्ट-समुन्नत नारी-समाज ने घर की दहलीज का उल्लंघन अवश्य किया है, पर ऐसा करके उसने रावण के द्वारा हरण किए जाने ही का खतरा उठाया है। ‘पुरुष’ यह छद्मवेशी राक्षस—साधु के वेश में भिक्षा के मिस उसे हरण करने की ताक में है। नारी को—उसके साहस ने, शिक्षा ने, समुन्नत होने से तनिक भी तो सहारा नहीं दिया है। बन्धुवर मैथिलीशरण गुप्त ने तो एक ही वाक्य में नारी का सब-कुछ बखान कर दिया—‘‘आँचल में है दूध, और आँखों में पानी।’’ अब वह नारी धन-दौलत, शिक्षा और सारी विभूतियों से लदी-फदी रहे, उसका सच्चा परिचय तो यही है—‘‘आँचल में है दूध और आँखों में पानी।’’
मैं तो पहले ही कह चुका हूँ—इस पानी में मैंने भी अपनी आँख का बहुत पानी मिलाया है, अलबत्ता, इसका कोई साक्षी नहीं है, परन्तु यह दूध का ऋण नहीं है, यह तो मेरे ‘जीवन’ का ऋण है। मैं तो यही समझता हूँ, और क्या समझते हैं—मैं नहीं जानता।
मैं चिकित्सक भी तो हूँ। और पचास वर्षों के अनुभव से मैंने एक चिकित्सा-तत्त्व पाया है, ‘विषस्य विषमौषधम्।’ यह बड़ा भारी गूढ़ तत्त्व है।
इसी तत्त्व पर मैंने ‘नारी-समस्या’ को भी परखा है। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच हूँ कि नारी ही नारी की समस्या को हल कर सकती है, परन्तु ‘नारी’ रहकर। ‘नर बनकर नहीं।’ ‘नारी’ बनने के लिए उसे ‘नारी-तत्त्व’ को जीवन में आत्मसात् करना होगा। ऐसा करने ही से वह, ‘अपराजिता’ के रूप में उदय होगी।
बीस बरस से मैं इस ‘अपराजिता’ नारी की खोज में था—कहीं मिलती ही न थी। इस बार जुलाई मास में बनारस गया। सख्त गर्मी थी, पंखा पास न था। बिस्तर भी नाकाफी था। मस्तिष्क में अनेक उलझनें भरी हुई थीं। वर्षा नहीं हो रही थी, हवा नहीं चल रही थी। खुली छत सोने के लिए नहीं थी। सब जड़-जंगम सरंजाम ऐसे जुट गए थे कि ‘निन्दिया रानी’ आई ही नहीं। अकस्मात् उस अर्ध निशा में ‘राज’ से साक्षात् हुआ। ‘ब्रज’ और ‘राधा’ उसी के साथ थे। तीनों बातें करने लगे। तीनों नहीं दोनों—‘राज’ और ‘राधा’। ब्रज सुनता था, केवल हँसता था। मैं भी सुनने लगा। सब बातें पते की थीं। कलम मेरे पास थी—और कागज भी। जो कुछ सुना, लिख डाला। और तब मैंने देखा—ओह, यह ‘राज’ तो सारे संसार की सभ्य-असभ्य नारियों से पृथक् अकेली ही खड़ी है। केवल अपनी ही सामर्थ्य पर। वह असहाय नहीं है, परमुखापेक्षी नहीं है—क्रोध, दैन्य, आवेश अधैर्य, सबसे पाक-साफ है। वह संयम-कर्तव्य और जीवन के सच्चे तत्त्वों की अधिष्ठात्री है। वह आज की नारी-मात्र की पथ-प्रदर्शिका है। मैंने उसे अपराजिता स्वीकार कर लिया। और उस दिन ‘ब्रजराज’ ने राज के चले जाने के बाद—जब उस भूमि पर—जहाँ उसके चरण-चिह्न बने थे—साष्टांग भू-पात करके अपना मस्तक टेक दिया—तो सबकी नजर बचाकर मैंने भी उन चरण-चिह्नों की एक कोर चूम ली। और मेरा अब तक का जीवन धन्य हो गया।
-चतुरसेन
1
राज का पत्र पाकर ब्रजराज बड़ी उलझन में पड़
गया। पत्र एक
निमन्त्रण मात्र था, उसमें केवल इतना ही लिखा था कि आज शाम को तुम्हारा
निमन्त्रण है, निमन्त्रण जरा लम्बा होगा, खूब फुरसत से आना ! ब्रजराज आज
की सन्ध्या की गाड़ी से घर जा रहा था, सब सामान बाँध-बूँध चुका था। कल राज
से वह घर जाने की विदाई ले आया था, अब यह अकस्मात् निमन्त्रण कैसा ?
परन्तु राज का निमन्त्रण नहीं टाला जा सकता था। ब्रजराज को घर जाना स्थगित
कर देना पड़ा और वह सन्ध्या होने से कुछ पहले ही राज के घर की ओर चल पड़ा।
ब्रजराज को देखते ही राज बराण्डे में निकल आई। उसने हँसकर कहा--‘‘बुरा तो बहुत लगा होगा, यात्रा में विघ्न पड़ गया।’’
‘‘लेकिन इस निमन्त्रण का अर्थ क्या है ?’’
‘‘अर्थ लम्बा है, समझने में देर लगेगी, भोजन में भी अभी देरी है, तब तक चलो वहाँ लॉन में बैठकर बात करें।’’
‘‘चलो !’’
दोनों लॉन में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। समय सुहावना था, क्षीण चन्द्रमा बादलों में से झाँक रहा था, और ठण्डी हवा चल रही थी। राज ने एक सफेद साड़ी पहनी थी। ब्रजराज ने कहा—‘‘अब कहो।’’
‘‘आप पूछिए !’’
‘‘आप ? आप कौन ?’’
‘‘आप ही, आप, और तो यहाँ है नहीं।’’
‘‘यह ‘आप’ कब से ?’’
‘‘आज से, बल्कि इसी क्षण से !’’
‘‘और यदि मैं अस्वीकार करूँ तो ?’’
‘‘तो आपसे अनुरोध करूँगी, प्रर्थना करूँगी।’’
‘‘खैर, देखा जाएगा, पहले निमन्त्रण की बात कहो। कल ही मैं तुमसे घर जाने की अनुमति ले गया था। यह असमय का निमन्त्रण कैसा ?’’
‘‘यह निमन्त्रण दो आदमियों के बीच मैत्री भाव स्थापित करने के उपलक्ष्य में है।’’
‘‘दो आदमी कौन ?’’
‘‘एक मैं और दूसरे आप।’’
‘‘फिर ‘आप’ ?’’
‘‘क्यों नहीं, आप मेरे गुरु नहीं ? अध्यापक नहीं ? शास्ता नहीं ?’’
‘‘तुम यह क्या पागलपन की बात कर रही हो, तुम्हारी हालत क्या है ? मुझे तुम्हारी बातचीत और हास्य सबमें एक नयापन दीख रहा है।’’
‘‘समय पर सब पुराना हो जाएगा। आप सह जाएँगे, और मैं भी।’’
‘‘तुम्हें मेरी कसम राज, साफ-साफ कहो मामला क्या है ?’’
‘‘साफ-साफ कहने से कोई लाभ नहीं है, जितना आवश्यक है उतना ही कहूँगी।’’
‘‘उतना ही कहो !’’
‘‘तो आज से हम—मैं और आप, जहाँ जिस अवस्था में रहें, परस्पर एक-दूसरे के सच्चे मित्र, शुभचिन्तक और सहायक की भाँति रहेंगे। जब तक कि जीवन है।’’
‘‘यह तुम क्या कह रही हो ?’’
‘‘और अब तक मेरे-आपके बीच जो बातें भावी जीवन के सम्बन्ध में हुईं,--हम लोगों ने जो मनसूबे बाँधे थे, वे इसी क्षण से समाप्त –विस्मृत समझे जाएँगे।’’
ब्रजराज उठकर खड़ा हो गया। उसने राज के हाथों को छूकर कहा—‘‘तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है, अच्छा हो यदि तुम आराम करो, और मैं जाऊँ।’’
‘‘किन्तु अभी बातें तो बहुत-सी बाकी हैं, और भोजन भी तैयार नहीं हुआ है, अभी आप जा न सकेंगे। मैंने तो लिख ही दिया था कि निमन्त्रण जरा लम्बा होगा।’’
‘‘लेकिन मैं यह कैसे जान सकता था कि आज तुम पागलों जैसी बातें करोगी !’’
‘‘पागलों—जैसी बातें नहीं कर रही हूँ। मैं जो कुछ कह रही हूँ उस पर मैंने खूब सोच-विचार लिया है।’’
‘‘तो पहेलियाँ न बुझाओ राज, जो कहना है एकदम कह दो !’’
‘‘एकदम ? क्या आपने मुझे कभी ऐसा निष्ठुर देखा था ?’’
‘‘परन्तु आज तो तुम्हारे रंग-ढंग ही निष्ठुर प्रतीत हो रहे हैं।’’
‘‘ऐसा नहीं है, मैं तो वही राज हूँ, जिसे आप भीतर से बाहर तक जान चुके हैं, और वह साहस, जिसका आज इस समय सहारा लेकर मैंने आपको निमन्त्रित किया है, आप ही का दिया हुआ है।’’
‘‘तो तुम्हारा यह मतलब तो नहीं है कि आज से हम-तुम दो हैं ?’’
‘‘हाँ, परन्तु दो ऐसे—जो परस्पर अकपट मित्र हैं, हृदय के इस पार से उस पार तक।’’
‘‘कल ही मैं तुमसे मिलकर गया था, इसी बीच यह सब हो गया ?’’
‘‘कभी-कभी शताब्दियाँ क्षणों में बीत जाती हैं, और कभी एक-एक क्षण वर्षों के समान हो जाता है। यह आप ही तो कहा करते हैं।’’
‘‘तो एक दिन-रात ही में शताब्दियाँ बीत गईं ? हम-तुम दोनों जो कल थे, आज वे न रहे ? दूसरा जन्म धारण कर चुके हैं ?’’
‘‘दूसरा ही क्यों, मैं तो कल से अब तक सैकड़ों बार मर कर जी चुकी। मेरे तो सैकड़ों जन्म हो चुके हैं।’’
‘‘तब मैं बाबूजी के पास जाता हूँ।’’
‘‘नहीं, जो कुछ कहना है मुझ ही से कहिए—और जो कुछ सुनना है मुझ ही से सुनिए !’’
‘‘मुझे कहना कुछ नहीं है, तुम जो सुनाना चाहती हो वह झटपट सुना दो !’’
‘‘अच्छा, तो सुनिए—इसी मास में मेरा विवाह ठाकुर साहब से हो रहा है, उन्हें तो आप जानते ही हैं ?’’
‘‘ब्रजराज के चेहरा सफेद बर्फ के समान हो गया। वह एकटक राज के मुँह की ओर ताकता बैठा रहा।
‘‘कुछ कहना चाहते हैं आप ?’’ राज ने मरी हुई आवाज में कहा।
‘‘न।’’
‘‘यह अच्छा है, अब सुनिए। मैंने इस काम के लिए अपने को केवल एक दिन में तैयार कर लिया, अब आप कितना समय लेंगे ?’’
‘‘मुझे क्या करना होगा राज ?’’
‘‘पिछली सारी बातें भूल जानी होंगी, मन का दुख धो बहाना होगा, और अब तक हम लोग खुश-खुश जैसे मिलते रहे हैं वैसे ही मिलते रहना होगा।’’
‘‘देखता हूँ, मैं तुम्हारे समान साहसी नहीं हूँ।’’
‘‘आप मेरे गुरु हैं, शिक्षक हैं, आप मुझसे पीछे न रह सकेंगे; जिस काम में मुझे पूरा दिन लगा है वह आपको कुछ मिनटों ही में कर डालना होगा।’’
‘‘क्या काम है वह ?’’
‘‘मन का बोझ एकदम उतार फेंकना होगा और इस नए सम्बन्ध का अभिनन्दन करना होगा।’’
‘‘तो राज, तुम अपना बल मुझे दो, मैं तो यह चोट सहन न कर सकूँगा। या तो मेरा प्राण ही निकल जाएगा या विक्षिप्त हो जाऊँगा। यह मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित रह सकता हूँ।’’
‘‘जब मैं सह सकती हूँ तो आपको भी सहना होगा। मैंने तो सारा साहस आप ही के भरोसे किया है, आप सहारा न देंगे तो मैं डगमगा जाऊँगी।’’
‘‘किन्तु राज, जो बात तुम नहीं बताना चाहतीं, वह मैं जानना भी नहीं चाहता। यह मैं समझता हूँ कि तुम्हारी इस निर्णय का कोई बहुत ही भारी कारण होगा लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे जीवन का सारा ही सहारा तुम हो !’’
‘‘उसी प्रकार मेरा सारा ही साहस आप पर निर्भर है। मैंने जो निर्णय किया है उसे मैं आपकी सहायता के बिना तो निभा न सकूँगी। अब मैं आपकी शरणागत हूँ।’’ उसका स्वर काँपा और शायद आँखें भी गीली हो गईं।
‘‘मुझे क्या करने को कहती हो राज ?’’
‘‘सम्भव है, आपको मुझसे अधिक कठिनाई पड़े। पर आप हैं भी तो महाशक्ति-पुंज। मेरे अन्दर जो शक्ति है, वह तो आप ही की दी हुई है। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन के कर्तव्य-भार को निबाह सकूँ।’’
‘‘आशीर्वाद देता हूँ राज !’’
‘‘विवाह में आपको उपस्थित रहकर सब कामों में हाथ बँटाना होगा।’’
‘‘अच्छा !’’
‘‘और उसके साथ एक अच्छी-सी लड़की ठीक करके—समझते हैं न आप ? पसन्द मैं करूँगी, और मैं ही ब्याह का सारा सरंजाम भी करूँगी।’’
‘‘इस बन्धन में क्यों बाँधती हो, पहली बात ही काफी है।’’
‘‘काफी नहीं है, जीवन-संग्राम लड़ना होगा, इस जीवन-संग्राम में पुरुष का शस्त्र स्त्री है और स्त्री का शस्त्र पुरुष। आप बिना शस्त्र लड़ेंगे कैसे ?’’
‘‘और यदि मैं लड़ने ही से इन्कार करूँ ?’’
‘‘वह तो अब समय ही बीत चुका, आपको लड़ना होगा !’’
‘‘तो राज, जैसा तुम कहोगी मैं वही करूँगा।’’
‘‘ईश्वर आपको चिरायु करे !’’
‘‘तो अब जाऊँ ?’’
‘‘वाह, भोजन तो अभी हुआ ही नहीं, जाओगे कैसे ! लेकिन उदास क्यों हो गए ?’’
‘‘धीरे-धीरे ही तो सहन होगा।’’
‘‘घर कब जाएँगे ?’’
‘‘अब नहीं जाऊँगा, छुट्टियों में यहीं रहूँगा। ब्याह के काम-काज में बाबूजी का हाथ बटाऊँगा। तुमने कहा न—इसी मास में।’’ ब्रजराज ने सूनी दृष्टि से राज की ओर देखा।
‘‘हाँ, वह तो है; परन्तु एक बार आपको घर तो जाना ही पड़ेगा।’’
‘‘किसलिए ?’’
‘‘पिताजी से बातें करने, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाबूजी ने उन्हें कल ही खत लिख दिया था।’’
‘‘खत तो मैंने भी लिखा था। कल यहाँ से जाने के बाद ही मुझे उनका खत मिला था, उसमें उन्होंने आवश्यक सामान की फहरिस्त लिख भेजी थी, और वे सब चीजें खरीदकर ले आने की आज्ञा दी थी।’’
‘‘आपने खरीद लीं वे सब चीजें ?’’
‘‘आज दिन-भर इसी काम में तो हम लोग जुटे रहे, मैं और भूपेन्द्र।’’
‘‘भूपेन्द्र, वह आपको कहाँ मिला ? है कहाँ वह ?’’
‘‘वहीं है, सब बाँध-बूँध रहा है, मैं तुमसे पूछना ही चाह रहा था कि भूपेन्द्र को दो दिन के लिए घर ले जाऊँगा।’’
‘‘उसे आपने इस काम में साथ क्यों लिया ?’’
‘‘उसने कल हमारी सब बातचीत सुन ली थी। आज सुबह ही वह मेरे पास आ पहुँचा। बोला—‘जीजी की पसन्द मैं जानता हूँ। साड़ियाँ और जेवर सब मैं अपनी पसन्द के खरीदूँगा’ बस, मैंने साथ ले लिया।’’ भूपेन्द्र ने जो उन्हें ‘‘जीजाजी’ कहकर सम्बोधित किया था वह सम्बोधन उनके मुँह से बाहर नहीं निकला।
‘‘इसी से आज वह मुझे दीखा ही नहीं।’’ राज के होंठ फड़के। कुछ रुककर उसने कहा—‘‘वापस भी तो हो सकती हैं ये सब चीजें।’’ उसका कण्ठ-कण्ठ-स्वर काँप गया।
‘‘खैर, देखा जाएगा; लेकिन पिताजी से क्या कहना होगा ?’’
‘‘उनसे तो यही कहना होगा कि किन्हीं कारणों से आपने ही विवाह का विचार स्थगित कर दिया है।’’
‘‘क्या मैं ऐसा लिखूँ ?’’
‘‘नहीं तो बाबूजी की मान-मार्यादा नहीं रहेगी, उन्होंने स्वयं पिताजी को वाग्दान दिया था। कल जो खत लिखा है उसमें ब्याह की तारीख भी लिख दी है। अब क्या उन्हीं की ओर से इन्कार जाएगा ? पिताजी भी यह कैसे सहेंगे, और बाबूजी तो जान दे देंगे, वचन-भंग नहीं करेंगे।’’ राज ने जैसे आर्तनाद किया।
ब्रजराज सोच में पड़ गया। उसने आँख उठाकर राज को देखा। राज का मुँह राख के समान निस्तेज हो रहा था, और आँखें पथरा रही थीं। ब्रजराज ने घबराकर खोए-से स्वर में कहा—‘‘चिन्ता मत करो राज, मैं सब ठीक कर लूँगा।’’
‘‘तो आप घर जाएँगे ?’’
‘‘नहीं, जा न सकूँगा, पिताजी को पत्र लिख दूँगा। सामने जाकर तो शायद मुझसे कुछ कहते-सुनते न बन पड़े। उन....’’ ब्रजराज एकाएक चुप होकर राज का मुँह ताकने लगा।
राजवती ने शंकित स्वर में कहा—‘‘और क्या बात है ?’’ ‘‘कुछ नहीं, पिताजी ने उन व्यक्तियों की भी फहरिस्त भेजी है, जिन्हें निमन्त्रण भेजे जा चुके हैं, और जिन्हें निमन्त्रण भेजे जाएँगे उनके नाम पूछे थे।’’ ब्रज ने नीची निगाह करके धीरे से कहा।
राज चुपचाप बैठी रही। उसकी आँखों से आँसू बह चले।
ब्रजराज ने हँसकर कहा—‘‘एक और बात भी लिखी थी पिताजी ने राज !’’
‘‘राज बोली नहीं। आँसू-भरे पलक उठाकर आँखों ही में प्रश्न किया।
ब्रजराज बहुत इच्छा रखते हुए भी हँस न सका। उसकी आँखें भी भर आईं।
राज ने पूछा—‘‘और क्या लिखा है पिताजी ने ?’’
‘‘लिखा है, सब काम बिटिया से और बाबूजी से पूछकर करना !’’
एक गहरा साँस छोड़कर ब्रजराज एकदम उठ खड़ा हुआ। उसने कहा--‘‘राज, देखो अब भोजन में देर कितनी है।’’
पर राज एकदम मूर्छित होकर कुर्सी से नीचे लुढ़क गई। ब्रजराज ने घबराकर उसे उठाया और कुर्सी पर बैठाकर रुमाल से उसके मुँह पर हवा की। कुछ ही क्षणों में राजवती ने होश में आकर ब्रजराज की ओर देखा। ब्रजराज ने दुखित स्वर में कहा—‘‘साहस करो राज, नहीं तो मुझसे भी कुछ करते-धरते न बनेगा।’’
राज का सब अंग काँप रहा था। वह बोली नहीं। धीरे से कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ब्रजराज ने उसे हाथ का सहारा देकर कहा—‘‘चलो देखें, भोजन में कितनी देर है।’’
‘‘दोनों धीरे-धीरे सीढ़ी चढ़कर कमरे में आए।
ब्रजराज को देखते ही राज बराण्डे में निकल आई। उसने हँसकर कहा--‘‘बुरा तो बहुत लगा होगा, यात्रा में विघ्न पड़ गया।’’
‘‘लेकिन इस निमन्त्रण का अर्थ क्या है ?’’
‘‘अर्थ लम्बा है, समझने में देर लगेगी, भोजन में भी अभी देरी है, तब तक चलो वहाँ लॉन में बैठकर बात करें।’’
‘‘चलो !’’
दोनों लॉन में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। समय सुहावना था, क्षीण चन्द्रमा बादलों में से झाँक रहा था, और ठण्डी हवा चल रही थी। राज ने एक सफेद साड़ी पहनी थी। ब्रजराज ने कहा—‘‘अब कहो।’’
‘‘आप पूछिए !’’
‘‘आप ? आप कौन ?’’
‘‘आप ही, आप, और तो यहाँ है नहीं।’’
‘‘यह ‘आप’ कब से ?’’
‘‘आज से, बल्कि इसी क्षण से !’’
‘‘और यदि मैं अस्वीकार करूँ तो ?’’
‘‘तो आपसे अनुरोध करूँगी, प्रर्थना करूँगी।’’
‘‘खैर, देखा जाएगा, पहले निमन्त्रण की बात कहो। कल ही मैं तुमसे घर जाने की अनुमति ले गया था। यह असमय का निमन्त्रण कैसा ?’’
‘‘यह निमन्त्रण दो आदमियों के बीच मैत्री भाव स्थापित करने के उपलक्ष्य में है।’’
‘‘दो आदमी कौन ?’’
‘‘एक मैं और दूसरे आप।’’
‘‘फिर ‘आप’ ?’’
‘‘क्यों नहीं, आप मेरे गुरु नहीं ? अध्यापक नहीं ? शास्ता नहीं ?’’
‘‘तुम यह क्या पागलपन की बात कर रही हो, तुम्हारी हालत क्या है ? मुझे तुम्हारी बातचीत और हास्य सबमें एक नयापन दीख रहा है।’’
‘‘समय पर सब पुराना हो जाएगा। आप सह जाएँगे, और मैं भी।’’
‘‘तुम्हें मेरी कसम राज, साफ-साफ कहो मामला क्या है ?’’
‘‘साफ-साफ कहने से कोई लाभ नहीं है, जितना आवश्यक है उतना ही कहूँगी।’’
‘‘उतना ही कहो !’’
‘‘तो आज से हम—मैं और आप, जहाँ जिस अवस्था में रहें, परस्पर एक-दूसरे के सच्चे मित्र, शुभचिन्तक और सहायक की भाँति रहेंगे। जब तक कि जीवन है।’’
‘‘यह तुम क्या कह रही हो ?’’
‘‘और अब तक मेरे-आपके बीच जो बातें भावी जीवन के सम्बन्ध में हुईं,--हम लोगों ने जो मनसूबे बाँधे थे, वे इसी क्षण से समाप्त –विस्मृत समझे जाएँगे।’’
ब्रजराज उठकर खड़ा हो गया। उसने राज के हाथों को छूकर कहा—‘‘तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है, अच्छा हो यदि तुम आराम करो, और मैं जाऊँ।’’
‘‘किन्तु अभी बातें तो बहुत-सी बाकी हैं, और भोजन भी तैयार नहीं हुआ है, अभी आप जा न सकेंगे। मैंने तो लिख ही दिया था कि निमन्त्रण जरा लम्बा होगा।’’
‘‘लेकिन मैं यह कैसे जान सकता था कि आज तुम पागलों जैसी बातें करोगी !’’
‘‘पागलों—जैसी बातें नहीं कर रही हूँ। मैं जो कुछ कह रही हूँ उस पर मैंने खूब सोच-विचार लिया है।’’
‘‘तो पहेलियाँ न बुझाओ राज, जो कहना है एकदम कह दो !’’
‘‘एकदम ? क्या आपने मुझे कभी ऐसा निष्ठुर देखा था ?’’
‘‘परन्तु आज तो तुम्हारे रंग-ढंग ही निष्ठुर प्रतीत हो रहे हैं।’’
‘‘ऐसा नहीं है, मैं तो वही राज हूँ, जिसे आप भीतर से बाहर तक जान चुके हैं, और वह साहस, जिसका आज इस समय सहारा लेकर मैंने आपको निमन्त्रित किया है, आप ही का दिया हुआ है।’’
‘‘तो तुम्हारा यह मतलब तो नहीं है कि आज से हम-तुम दो हैं ?’’
‘‘हाँ, परन्तु दो ऐसे—जो परस्पर अकपट मित्र हैं, हृदय के इस पार से उस पार तक।’’
‘‘कल ही मैं तुमसे मिलकर गया था, इसी बीच यह सब हो गया ?’’
‘‘कभी-कभी शताब्दियाँ क्षणों में बीत जाती हैं, और कभी एक-एक क्षण वर्षों के समान हो जाता है। यह आप ही तो कहा करते हैं।’’
‘‘तो एक दिन-रात ही में शताब्दियाँ बीत गईं ? हम-तुम दोनों जो कल थे, आज वे न रहे ? दूसरा जन्म धारण कर चुके हैं ?’’
‘‘दूसरा ही क्यों, मैं तो कल से अब तक सैकड़ों बार मर कर जी चुकी। मेरे तो सैकड़ों जन्म हो चुके हैं।’’
‘‘तब मैं बाबूजी के पास जाता हूँ।’’
‘‘नहीं, जो कुछ कहना है मुझ ही से कहिए—और जो कुछ सुनना है मुझ ही से सुनिए !’’
‘‘मुझे कहना कुछ नहीं है, तुम जो सुनाना चाहती हो वह झटपट सुना दो !’’
‘‘अच्छा, तो सुनिए—इसी मास में मेरा विवाह ठाकुर साहब से हो रहा है, उन्हें तो आप जानते ही हैं ?’’
‘‘ब्रजराज के चेहरा सफेद बर्फ के समान हो गया। वह एकटक राज के मुँह की ओर ताकता बैठा रहा।
‘‘कुछ कहना चाहते हैं आप ?’’ राज ने मरी हुई आवाज में कहा।
‘‘न।’’
‘‘यह अच्छा है, अब सुनिए। मैंने इस काम के लिए अपने को केवल एक दिन में तैयार कर लिया, अब आप कितना समय लेंगे ?’’
‘‘मुझे क्या करना होगा राज ?’’
‘‘पिछली सारी बातें भूल जानी होंगी, मन का दुख धो बहाना होगा, और अब तक हम लोग खुश-खुश जैसे मिलते रहे हैं वैसे ही मिलते रहना होगा।’’
‘‘देखता हूँ, मैं तुम्हारे समान साहसी नहीं हूँ।’’
‘‘आप मेरे गुरु हैं, शिक्षक हैं, आप मुझसे पीछे न रह सकेंगे; जिस काम में मुझे पूरा दिन लगा है वह आपको कुछ मिनटों ही में कर डालना होगा।’’
‘‘क्या काम है वह ?’’
‘‘मन का बोझ एकदम उतार फेंकना होगा और इस नए सम्बन्ध का अभिनन्दन करना होगा।’’
‘‘तो राज, तुम अपना बल मुझे दो, मैं तो यह चोट सहन न कर सकूँगा। या तो मेरा प्राण ही निकल जाएगा या विक्षिप्त हो जाऊँगा। यह मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित रह सकता हूँ।’’
‘‘जब मैं सह सकती हूँ तो आपको भी सहना होगा। मैंने तो सारा साहस आप ही के भरोसे किया है, आप सहारा न देंगे तो मैं डगमगा जाऊँगी।’’
‘‘किन्तु राज, जो बात तुम नहीं बताना चाहतीं, वह मैं जानना भी नहीं चाहता। यह मैं समझता हूँ कि तुम्हारी इस निर्णय का कोई बहुत ही भारी कारण होगा लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे जीवन का सारा ही सहारा तुम हो !’’
‘‘उसी प्रकार मेरा सारा ही साहस आप पर निर्भर है। मैंने जो निर्णय किया है उसे मैं आपकी सहायता के बिना तो निभा न सकूँगी। अब मैं आपकी शरणागत हूँ।’’ उसका स्वर काँपा और शायद आँखें भी गीली हो गईं।
‘‘मुझे क्या करने को कहती हो राज ?’’
‘‘सम्भव है, आपको मुझसे अधिक कठिनाई पड़े। पर आप हैं भी तो महाशक्ति-पुंज। मेरे अन्दर जो शक्ति है, वह तो आप ही की दी हुई है। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन के कर्तव्य-भार को निबाह सकूँ।’’
‘‘आशीर्वाद देता हूँ राज !’’
‘‘विवाह में आपको उपस्थित रहकर सब कामों में हाथ बँटाना होगा।’’
‘‘अच्छा !’’
‘‘और उसके साथ एक अच्छी-सी लड़की ठीक करके—समझते हैं न आप ? पसन्द मैं करूँगी, और मैं ही ब्याह का सारा सरंजाम भी करूँगी।’’
‘‘इस बन्धन में क्यों बाँधती हो, पहली बात ही काफी है।’’
‘‘काफी नहीं है, जीवन-संग्राम लड़ना होगा, इस जीवन-संग्राम में पुरुष का शस्त्र स्त्री है और स्त्री का शस्त्र पुरुष। आप बिना शस्त्र लड़ेंगे कैसे ?’’
‘‘और यदि मैं लड़ने ही से इन्कार करूँ ?’’
‘‘वह तो अब समय ही बीत चुका, आपको लड़ना होगा !’’
‘‘तो राज, जैसा तुम कहोगी मैं वही करूँगा।’’
‘‘ईश्वर आपको चिरायु करे !’’
‘‘तो अब जाऊँ ?’’
‘‘वाह, भोजन तो अभी हुआ ही नहीं, जाओगे कैसे ! लेकिन उदास क्यों हो गए ?’’
‘‘धीरे-धीरे ही तो सहन होगा।’’
‘‘घर कब जाएँगे ?’’
‘‘अब नहीं जाऊँगा, छुट्टियों में यहीं रहूँगा। ब्याह के काम-काज में बाबूजी का हाथ बटाऊँगा। तुमने कहा न—इसी मास में।’’ ब्रजराज ने सूनी दृष्टि से राज की ओर देखा।
‘‘हाँ, वह तो है; परन्तु एक बार आपको घर तो जाना ही पड़ेगा।’’
‘‘किसलिए ?’’
‘‘पिताजी से बातें करने, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाबूजी ने उन्हें कल ही खत लिख दिया था।’’
‘‘खत तो मैंने भी लिखा था। कल यहाँ से जाने के बाद ही मुझे उनका खत मिला था, उसमें उन्होंने आवश्यक सामान की फहरिस्त लिख भेजी थी, और वे सब चीजें खरीदकर ले आने की आज्ञा दी थी।’’
‘‘आपने खरीद लीं वे सब चीजें ?’’
‘‘आज दिन-भर इसी काम में तो हम लोग जुटे रहे, मैं और भूपेन्द्र।’’
‘‘भूपेन्द्र, वह आपको कहाँ मिला ? है कहाँ वह ?’’
‘‘वहीं है, सब बाँध-बूँध रहा है, मैं तुमसे पूछना ही चाह रहा था कि भूपेन्द्र को दो दिन के लिए घर ले जाऊँगा।’’
‘‘उसे आपने इस काम में साथ क्यों लिया ?’’
‘‘उसने कल हमारी सब बातचीत सुन ली थी। आज सुबह ही वह मेरे पास आ पहुँचा। बोला—‘जीजी की पसन्द मैं जानता हूँ। साड़ियाँ और जेवर सब मैं अपनी पसन्द के खरीदूँगा’ बस, मैंने साथ ले लिया।’’ भूपेन्द्र ने जो उन्हें ‘‘जीजाजी’ कहकर सम्बोधित किया था वह सम्बोधन उनके मुँह से बाहर नहीं निकला।
‘‘इसी से आज वह मुझे दीखा ही नहीं।’’ राज के होंठ फड़के। कुछ रुककर उसने कहा—‘‘वापस भी तो हो सकती हैं ये सब चीजें।’’ उसका कण्ठ-कण्ठ-स्वर काँप गया।
‘‘खैर, देखा जाएगा; लेकिन पिताजी से क्या कहना होगा ?’’
‘‘उनसे तो यही कहना होगा कि किन्हीं कारणों से आपने ही विवाह का विचार स्थगित कर दिया है।’’
‘‘क्या मैं ऐसा लिखूँ ?’’
‘‘नहीं तो बाबूजी की मान-मार्यादा नहीं रहेगी, उन्होंने स्वयं पिताजी को वाग्दान दिया था। कल जो खत लिखा है उसमें ब्याह की तारीख भी लिख दी है। अब क्या उन्हीं की ओर से इन्कार जाएगा ? पिताजी भी यह कैसे सहेंगे, और बाबूजी तो जान दे देंगे, वचन-भंग नहीं करेंगे।’’ राज ने जैसे आर्तनाद किया।
ब्रजराज सोच में पड़ गया। उसने आँख उठाकर राज को देखा। राज का मुँह राख के समान निस्तेज हो रहा था, और आँखें पथरा रही थीं। ब्रजराज ने घबराकर खोए-से स्वर में कहा—‘‘चिन्ता मत करो राज, मैं सब ठीक कर लूँगा।’’
‘‘तो आप घर जाएँगे ?’’
‘‘नहीं, जा न सकूँगा, पिताजी को पत्र लिख दूँगा। सामने जाकर तो शायद मुझसे कुछ कहते-सुनते न बन पड़े। उन....’’ ब्रजराज एकाएक चुप होकर राज का मुँह ताकने लगा।
राजवती ने शंकित स्वर में कहा—‘‘और क्या बात है ?’’ ‘‘कुछ नहीं, पिताजी ने उन व्यक्तियों की भी फहरिस्त भेजी है, जिन्हें निमन्त्रण भेजे जा चुके हैं, और जिन्हें निमन्त्रण भेजे जाएँगे उनके नाम पूछे थे।’’ ब्रज ने नीची निगाह करके धीरे से कहा।
राज चुपचाप बैठी रही। उसकी आँखों से आँसू बह चले।
ब्रजराज ने हँसकर कहा—‘‘एक और बात भी लिखी थी पिताजी ने राज !’’
‘‘राज बोली नहीं। आँसू-भरे पलक उठाकर आँखों ही में प्रश्न किया।
ब्रजराज बहुत इच्छा रखते हुए भी हँस न सका। उसकी आँखें भी भर आईं।
राज ने पूछा—‘‘और क्या लिखा है पिताजी ने ?’’
‘‘लिखा है, सब काम बिटिया से और बाबूजी से पूछकर करना !’’
एक गहरा साँस छोड़कर ब्रजराज एकदम उठ खड़ा हुआ। उसने कहा--‘‘राज, देखो अब भोजन में देर कितनी है।’’
पर राज एकदम मूर्छित होकर कुर्सी से नीचे लुढ़क गई। ब्रजराज ने घबराकर उसे उठाया और कुर्सी पर बैठाकर रुमाल से उसके मुँह पर हवा की। कुछ ही क्षणों में राजवती ने होश में आकर ब्रजराज की ओर देखा। ब्रजराज ने दुखित स्वर में कहा—‘‘साहस करो राज, नहीं तो मुझसे भी कुछ करते-धरते न बनेगा।’’
राज का सब अंग काँप रहा था। वह बोली नहीं। धीरे से कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ब्रजराज ने उसे हाथ का सहारा देकर कहा—‘‘चलो देखें, भोजन में कितनी देर है।’’
‘‘दोनों धीरे-धीरे सीढ़ी चढ़कर कमरे में आए।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i