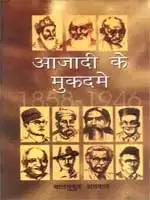|
विविध >> आजादी के मुकदमें आजादी के मुकदमेंबालमुकुन्द अग्रवाल
|
73 पाठक हैं |
|||||||
ब्रिटिश शासन के दौरान चलाये गये ये मुकदमे भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के 90 वर्षों (1858-1946) के इतिहास की कहानी कहते हैं।
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
ब्रिटिश शासन के दौरान चलाये गये ये मुकदमे भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के
90 वर्षों (1858-1946) के इतिहास की कहानी कहते हैं। पाठकों को इनसे उन
साहसी स्वतंत्रता सेनानियों के आत्मबल और चरित्र को समझने की गहरी
अंतर्दृष्टि मिलेगी, जिन्होंने देश के लिए अनेक कष्ट सहे और अपना सर्वस्य
त्याग दिया। इसके साथ ही, इन मुकदमों से तत्कालीन रक्तरंजित सामाजिक,
राजनीतिक और संवैधानिक परिस्थियों की भी जानकारी मिलगी, जिन्हें जानना
अपने साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को जानने के समान है। इस पुस्तक में
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बालगंगाधर तिलक, श्री अरविन्द, विनायक दामोदर सावरकर,
महात्मा गाँधी, सरदार भगत सिंह, एम.एन.राय सरीखे देश के प्रमुख देशभक्तों
पर चलाये गये मुकदमों की प्रामाणिक जानकारी दी गयी।
बालमुकुंद अग्रवाल (1926-92) ने इतिहास और समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् कानून की पढ़ाई की, और 1955 में बंबई विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाया। 1958 में उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील के रूप में 1959 में उनका नामांकन हुआ, जहाँ वह अपने अंतिम दिनों तक एक वरिष्ठ वकील के रूप में सक्रिय रहे।
बालमुकुंद अग्रवाल (1926-92) ने इतिहास और समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् कानून की पढ़ाई की, और 1955 में बंबई विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाया। 1958 में उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील के रूप में 1959 में उनका नामांकन हुआ, जहाँ वह अपने अंतिम दिनों तक एक वरिष्ठ वकील के रूप में सक्रिय रहे।
भूमिका
भारत में ब्रिटिश शासन के उत्थान और पतन के
युग को सहज ही दो भागों में
बांटा जा सकता है—1857 से पूर्व और 1858 से 1947 तक।
सन् 1857 से पहले का समय ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रसार तथा उसकी प्रभुसत्ता के अधीन छोटे-बड़े भारतीय शासकों की सत्ता की आपसी लड़ाइयों का समय है। ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीय सिपाही भी भारतीय शासकों की अपेक्षा ब्रिटिश अफसरों के प्रति ज्यादा वफादार थे, जिससे अंग्रेजों को भारतीय भूमि पर पांव जमाने में काफी मदद मिली।
सन् 1857 में पहली बार कुछ भारतीय देशभक्तों ने ब्रिटिश सत्ता को गिराने और उसके दमनकारी शासन से मुक्ति पाने के लिए संगठित होने का निर्णय लिया था। भारतीयों के लिए यह आजादी की लड़ाई थी, जबकि अंग्रेजों ने इसे बगावत या गदर का नाम दिया था। नाम कुछ भी हो, विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का यह पहला व्यवस्थित, सचेत और शक्तिशाली प्रयास था। हालांकि भारत तब एक प्रभुसत्ता-संपन्न देश कहलाता था, किंतु वास्तविकता यह थी कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह ज़फर सम्राट कहलाने के बावजूद अंग्रेजों से पेंशन पाते थे और दिल्ली के लाल किले चारदीवारी में कैद थे।
जब बहादुरशाह ज़फर को गिरफ्तार कर, मुकदमा चलाकर, दोषी ठहराया गया, तो कई जिलों में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। कुछ लोगों ने अकेले ही हथियार उठा लिए, तो कुछ ने दलों में संगठित होकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी।
सन् 1857 से 1947 के बीच के वर्षों में अनेक नेता सामने आये तथा कई राजनीतिक दलों का उत्कर्ष हुआ। कुछ ने संवैधानिक सुधारों के रास्ते स्वराज्य तक पहुंचने के लिए आंदोलन किया तो कुछ ने ‘डोमिनियन स्टेटस’ (स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दिए जाने) की मांग की। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो प्रतीक्षा के लिए तैयार न थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के साथ-साथ हथियार भी उठा लिये। उनमें से कुछ को अंग्रजों द्वारा मार दिया गया, तो कुछ को बिना मुकदमे चलाए ही निर्वासित कर दिया गया। भारतवासियों की आवाज दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा राजद्रोह के कानून को पूरी सख्ती से लागू किया गया।
जब मुझे पहली बार बहादुरशाह ज़फर और आजाद हिंद फौज के मुकदमों पर मोतीराम का संपूर्ण विवरण प्राप्त हुआ, तो उसे पढ़कर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। कारण, दोनों मुकदमों में अद्भुत समानता थी, चाहे वे लगाये गये आरोप हों या अपनायी गयी कार्यविधि, या फिर निकाले गये निष्कर्ष। पहला मुकदमा भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत करता था, तो दूसरा मुकदमा, लगभग 90 साल बाद ब्रिटिश साम्राज्य के अवसान की घोषणा की तरह था।
इस काल का सर्वेक्षण करने पर ऐसे कई क्रांतिकारियों, चिंतकों, पत्रकारों और राजनीतिक नेताओं के मुकदमें मेरे सामने आये, जिन्हें आजादी के लिए लड़ने के कारण दंड दिया गया था। इन्हीं मुकदमों ने जन-साधारण में राजनीतिक चेतना जगाने में अपूर्व योगदान दिया था। इन मुकदमों के अभियुक्त भिन्न प्रकृति और विचारधारा के लोग थे। अपनायी गयी कार्यविधि भी भिन्न थी। प्रधान न्यायाधीशों के मत, दृष्टिकोण तथा बचाव पक्ष के तर्क भी हर मुकदमें में अलग-अलग थे। भिन्न रूप-रंग के 11 मुकदमों का चयन कर मैंने उन्हें ऐसी पुस्तक का रूपाकार दिया है, जिससे भारत का इतिहास अभिव्यक्त होता है और जिसे हर भारतीय पड़ना पसंद करेगा।
क्रांतिकारियों के सिर्फ इतने ही मुकदमे नहीं हैं। इनके अतिरिक्त और कितने ही मुकदमे हैं, लेकिन इन कुछ मुकदमों को चुनने का कारण यह था कि वे भारत के स्वाधीनता-संग्राम का क्रमबद्ध इतिहास बताते हैं।
बहादुरशाह ज़फर का मुकदमा ऐतिहासिक लाल किले के भीतर चलाया गया पहला मुकदमा था, जिसमें एक सम्राट पर एक साधारण व्यक्ति की तरह राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायविधि के नियम-कानून का पूर्णतः उल्लंघन किया गया। एक सम्राट को न तो कोई सम्मान दिया गया, न प्रतिवाद के लिए न्यायिक सहयोग ही। सारे गवाह भी अंग्रेजी हुकूमत के ताबेदार थे। मुगल साम्राज्य का सूरज डूब रहा था। फिर भी, न्याय कैसे किया जाता था, यह दिखाने में इस मुकदमे की अपनी भूमिका है।
लोकमान्य गंगाधर तिलक को इस देश में कौन नहीं जानता। उन्हें ‘भारतीय स्वाधीनता संग्राम का पितामह’ कहा गया है, क्योंकि वही महात्मा गांधी को राजनीतिक रणभूमि में लाये थे। तिलक एक विद्वान, पत्रकार तथा लेखक थे, जो बराबर ब्रिटिश कुशासन, शोषण और पक्षपात के विरुद्ध लिखते रहे। इन उत्तेजक लेखों के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। तिलक ने अपना बचावनामा खुद लिखा और निडर होकर कहा : ‘आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।’ अदालत में कहा गया यह अंतिम वाक्य अमर हो चुका है और आज भी बंबई उच्च न्यायलय की इमारत के केंद्रीय कक्ष में अंकित है।
‘बंगाल का शेर’ कहलाने वाले सुरेन्द्रनाथ बनर्जी पर मुकदमा चालाया गया, जब उन्होंने एक अंग्रेज न्यायाधीश की आलोचना करने का साहस किया। उन्हें कारावास का दंड दिया गया, जिसका उन्होंने यह कहकर स्वागत किया कि ‘मुझे अपनी पीढ़ी और अपने रुतबे के पहले ऐसे भारतीय होने का गौरव मिला था, जिसे जन-कर्तव्य पालन के लिए कारावास का दंड झेलना पड़ा।’
अलीपुर बम-कांड में श्री अरविंद घोष का मुकदमा ऐसा राजकीय मुकदमा था, जिसमें अभियुक्त पर एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश अफसर के कत्ल की कोशिश करने, चूकने और दूसरे को मार बैठने का आरोप लगाया गया था। कालांतर में यह अभियुक्त भारत के प्रमुख संत, पैगंबर और आध्यात्मिक नेता बने, जबकि उनके बचाव वकील सी.आर. दास एक स्वाधीनता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध हुए। सी.आर. दास का बचाव-वक्तव्य बार-बार पढ़े जाने योग्य है। मैंने मुकदमे को मूल रूप में पढ़कर यही महसूस किया कि एक छोटे-से लेख में उनके प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करना काफी मुश्किल काम है। यह मुकदमा दो महान व्यक्तियों के उत्थान का कारण बना। पहले ने आध्यात्मिक संस्कृति को समृद्ध बनाया, तो दूसरे ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को ऊर्जा प्रदान की।
‘वीर सावरकर’ के नाम से प्रसिद्ध विनायक दामोदर सावरकर बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने विदेश में पढ़ते वक्त क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। उनकी गिरफ्तारी, निर्वासन, उनका फरार होना, तथा फ्रांसिसी पुलिस द्वारा पुनः बंदी बनाया जाना—एक नाटकीय कथा की तरह है। उनके मुकदमे तो इससे भी बढ़कर हैं। उन पर भारत में भी मुकदमा चलाया गया और ‘द हेग’ के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ निर्णय न्यायालय में भी, जिससे विदेशी शासन से मुक्ति की भारतीय आकांक्षाओं से सारा विश्व परिचित हुआ। इस मुकदमें में यह भी दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ निर्णय न्यायालय में अपने हक में फैसला कराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस तरह अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल किया।
महात्मा गांधी के ‘यंग इंडिया’ में प्रकाशित विवादास्पद लेखों के कारण उन पर और प्रकाशक शंकरलाल बेंकर पर चलाया गया मुकदमा न्यायाधीश की निष्पक्षता और सौजन्यता के कारण विश्व के न्यायिक इतिहास के आलेख में दर्ज है। मुख्य न्यायाधीश जे.एम. शेलेट ने लिखा है : ‘‘सुकरात के मुकदमे को छोड़कर पूरे मानव इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मुकदमा होगा, जिसने गांधीजी के मुकदमे की तरह इतना तहलका मचाया हो और मानव-जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाला हो। नियमों पर सत्य की विजय की यह एक मिसाल है। न्याय का सम्मान होना चाहिए, और एक न्यायाधीश को अपना फर्ज निभाना चाहिए।’’ मुकदमे के मुख्य न्यायाधीश के कथन भी उद्धत करने योग्य हैं : ‘‘मेरा मानना यह है कि आपको तिलक महोदय की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, अर्थात् हर अभियोग पर दो साल साधारण कारावास, कुल मिलाकर 6 साल। यही दंड आपको देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। लेकिन ऐसा करते वक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर भावी परिस्थितियों में सरकार आपकी सजा घटाने या आपको रिहा करने का निर्णय लेती है, तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी।’’
स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में सरदार भगत सिंह के मुकदमे का अपना विशिष्ट स्थान है। भगत सिंह और उसके साथियों द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने, सांडर्स नामक ब्रिटिश अफसर को मारने और फिर मुकदमे का सामना करने के साहसपूर्ण कार्य से स्वाधीनता संग्राम को एक नया आवेग मिला था। भगत सिंह ने अपने किये को न्यायोचित ठहराते हुए अपना बचावनामा खुद लिखा था, जिसे उनके वकील आसफ अली ने पढ़कर सुनाया था। वक्तव्य में कहा गया था : ‘‘इंग्लैंड को उसकी स्वप्न-निद्रा से जगाने के लिए बम फेंकना जरूरी था। असेंबली के बीच बम फेंककर हमने उन लोगों की तरफ से विरोध प्रकट किया, जिनके पास अपनी हार्दिक वेदना को व्यक्त करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारा एक मात्र उद्देश्य बहरों को सुनाना और असावधानों को वक्त रहते चेतावनी देना था।’’
लेबर पार्टी की हुकूमत के वक्त चलाया गया यह मुकदमा इस बात का प्रमाण है कि अंग्रेजी नीति ही आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन की थी, सरकार भले ही ‘लेबर’ की हो या ‘कंजरवेटिव्स’ की। इतना ही नहीं, भारत में ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था का एक ही उद्देश्य था—अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने वालों का दमन करना।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उभरती कुछ प्रवृत्तियों और कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती गतिविधियों को देखकर भी ब्रटिश शासन को काफी चिंता थी। बुद्धिजीवियों की एक बड़ी संख्या वाली कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा तथा श्रमिक वर्ग तक पहुंच गयी थी। फिर, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से भी खतरा था क्योंकि भारतीय कम्युनिस्टों का उससे गहरा संबंध था। उनकी विचार धारा भी वहीं से ली गयी थी। इसलिए कई प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया गया और ब्रिटिश प्रभुसत्ता के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। कायदे से मुकदमा वहीं चलाया जाना चाहिए था जहां जूरी उनका परीक्षण कर सके, लेकिन जूरी से बचने के लिए मुकदमे को मनमाने ढंग से उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थानांतरित कर दिया गया। अदालत ने जानबूझकर एक ऐसी विवादास्पद कार्यविधि का पालन किया, जिससे अभियुक्तों को दोषी ठहराया जा सके। यह मुकदमा चार साल तक खिंचा। सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारपत्रों में उसे छापा गया और ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था का हास्यास्पद चरित्र उजागर हो गया। श्रमिक वर्ग को संगठित करने में इस मुकदमे से बहुत सहायता मिली।
महान बुद्धिजीवी और क्रांतिकारी एम.एन. राय ‘कम्युनिस्ट इंटरनेशनल’ के संस्थापकों में एक थे। रूसी क्रांति के समय लेनिन के साथ काम करने वाले वह एकमात्र भारतीय थे। भारत के क्रांतिकारियों और उनकी गतिविधियों को एम.एन. राय का समर्थन मिलना ब्रिटिश सरकार के लिए गंभीर खतरा था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमे के समय वह विदेश में थे। सन् 1931 में भारत लौटने पर उन्हें नाटकीय परिस्थितियों में षड्यंत्र और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राय ने अपना बचावनामा खुद लिखा, जिसे उनके वकील ने पढ़कर सुनाया। यह बचावनामा एक साधारण शोध-प्रबंध है—शोषित, दीन-दुखियों के अधिकारों की प्रतिरक्षा करता हुआ, उन्हें अपनी गरीबी हटाने, शोषकों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता हुआ। एम.एन. राय ने भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का इतिहास कुरेदते हुए लिखा-‘‘सत्ता हथियाने वाली ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी लड़ाई का रास्ता ही भारत में संवैधानिक सरकार की स्थापना का एकमात्र रास्ता है।’’ बचाव की यह दलील सर्वाधिक न्यायोचित, तार्किक और सुसंगत दस्तावेजों में से एक है। भले ही उनके अपने बचाव में इसका इस्तेमाल न हो सका, लेकिन आजाद हिंद फौज (आई.एन.ए.) पर शेख अब्दुल्ला के मुकदमों की प्रतिवादी दलील तैयार करने में क्रमशः भूलाभाई देसाई और आसफ अली को इससे आधार और प्रेरणा मिली।
सन् 1945 में आजाद हिंद फौज के तीन अफसरों का मुकदमा ब्रिटिश सरकार के शक्ति-प्रदर्शन का अंतिम प्रयास था। जनमहत्व के मूलभूत मुद्दों को जोड़ते हुए सुप्रतिष्ठित वकीलों का एक दल भारतीय अफसरों के बचाव के लिए सामने आया। ‘हर राष्ट्र को अपनी आजादी के लिए लड़ने का अधिकार है’-यह तर्क ब्रिटिश सेना के विरुद्ध आजाद हिंद फौज के गठन को न्यायोचित ठहराता था। इस मुकदमें में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के व्यापक और नवीन पक्षों पर बहस हुई। देश को आजाद कराने की नेताजी की यह साहसपूर्ण कोशिश इतिहास में अपूर्व तो थी ही, हर भारतीय के लिए अद्भुत, आकर्षक और प्रेरणादायक भी थी। इस मुकदमे से भारत में ब्रटिश शासन का अंत हुआ।
इतिहास को पूरा करने के लिए शेख अब्दुल्ला के मुकदमे को भी इससे जोड़ दिया गया है। अंग्रेज देशी प्रांत में प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन शाही रियायतों में नवाबों के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन करते थे। देशी रियासतों के शासक अपनी प्रजा की जिंदगी, आजादी और संपत्ति पर असीमित निरंकुश सत्ता रखते थे। पराधीन भारत की कई देशी रियासतों में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए समानांतर आंदोलन हुए। देशी राजाओं ने इन आंदोलनों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कश्मीर के एक महत्वपूर्ण नेता शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के निरंकुश शासन के विरुद्ध कश्मीरियों को संगठित किया। सन् 1946 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, ये शासक अपनी रियासतें छोड़ने को तैयार न थे। शेख अब्दुल्ला ने महाराजा को गद्दी से हटाने के लिए कश्मीरवासियों का आह्वान किया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया।
सुप्रसिद्ध भारतीय वकील आसफ अली ने अन्य योग्य वकीलों के साथ मिलकर अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ा। हालांकि शेख अब्दुल्ला को दोषी ठहराया गया, लेकिन यह मुकदमा उनके लिए नैतिक विजय साबित हुआ और 1947 में वह कश्मीर के पहले ‘प्रिमीयर’ बने।
जिस तरह आजाद हिंद फौज मुकदमा भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करने वाला मुकदमा था, उसी तरह शेख अब्दुल्ला का मुकदमा देशी रियासतों में नवाबों के निरंकुश शासन का अंत कर पूर्ण स्वराज्य लाने का मुकदमा था।
ये मुकदमे एक तरह से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के 90 वर्षों के इतिहास की कथा कहते हैं। पाठकों को इनसे उन साहसी स्वतंत्रता-सेनानियों के चरित्र को समझने की गहरी अंतर्दृष्टि मिलेगी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हर चुनौती का सामना किया तथा अपना सर्वस्व त्याग दिया।
सन् 1857 से पहले का समय ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रसार तथा उसकी प्रभुसत्ता के अधीन छोटे-बड़े भारतीय शासकों की सत्ता की आपसी लड़ाइयों का समय है। ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीय सिपाही भी भारतीय शासकों की अपेक्षा ब्रिटिश अफसरों के प्रति ज्यादा वफादार थे, जिससे अंग्रेजों को भारतीय भूमि पर पांव जमाने में काफी मदद मिली।
सन् 1857 में पहली बार कुछ भारतीय देशभक्तों ने ब्रिटिश सत्ता को गिराने और उसके दमनकारी शासन से मुक्ति पाने के लिए संगठित होने का निर्णय लिया था। भारतीयों के लिए यह आजादी की लड़ाई थी, जबकि अंग्रेजों ने इसे बगावत या गदर का नाम दिया था। नाम कुछ भी हो, विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का यह पहला व्यवस्थित, सचेत और शक्तिशाली प्रयास था। हालांकि भारत तब एक प्रभुसत्ता-संपन्न देश कहलाता था, किंतु वास्तविकता यह थी कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह ज़फर सम्राट कहलाने के बावजूद अंग्रेजों से पेंशन पाते थे और दिल्ली के लाल किले चारदीवारी में कैद थे।
जब बहादुरशाह ज़फर को गिरफ्तार कर, मुकदमा चलाकर, दोषी ठहराया गया, तो कई जिलों में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। कुछ लोगों ने अकेले ही हथियार उठा लिए, तो कुछ ने दलों में संगठित होकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी।
सन् 1857 से 1947 के बीच के वर्षों में अनेक नेता सामने आये तथा कई राजनीतिक दलों का उत्कर्ष हुआ। कुछ ने संवैधानिक सुधारों के रास्ते स्वराज्य तक पहुंचने के लिए आंदोलन किया तो कुछ ने ‘डोमिनियन स्टेटस’ (स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दिए जाने) की मांग की। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो प्रतीक्षा के लिए तैयार न थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के साथ-साथ हथियार भी उठा लिये। उनमें से कुछ को अंग्रजों द्वारा मार दिया गया, तो कुछ को बिना मुकदमे चलाए ही निर्वासित कर दिया गया। भारतवासियों की आवाज दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा राजद्रोह के कानून को पूरी सख्ती से लागू किया गया।
जब मुझे पहली बार बहादुरशाह ज़फर और आजाद हिंद फौज के मुकदमों पर मोतीराम का संपूर्ण विवरण प्राप्त हुआ, तो उसे पढ़कर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। कारण, दोनों मुकदमों में अद्भुत समानता थी, चाहे वे लगाये गये आरोप हों या अपनायी गयी कार्यविधि, या फिर निकाले गये निष्कर्ष। पहला मुकदमा भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत करता था, तो दूसरा मुकदमा, लगभग 90 साल बाद ब्रिटिश साम्राज्य के अवसान की घोषणा की तरह था।
इस काल का सर्वेक्षण करने पर ऐसे कई क्रांतिकारियों, चिंतकों, पत्रकारों और राजनीतिक नेताओं के मुकदमें मेरे सामने आये, जिन्हें आजादी के लिए लड़ने के कारण दंड दिया गया था। इन्हीं मुकदमों ने जन-साधारण में राजनीतिक चेतना जगाने में अपूर्व योगदान दिया था। इन मुकदमों के अभियुक्त भिन्न प्रकृति और विचारधारा के लोग थे। अपनायी गयी कार्यविधि भी भिन्न थी। प्रधान न्यायाधीशों के मत, दृष्टिकोण तथा बचाव पक्ष के तर्क भी हर मुकदमें में अलग-अलग थे। भिन्न रूप-रंग के 11 मुकदमों का चयन कर मैंने उन्हें ऐसी पुस्तक का रूपाकार दिया है, जिससे भारत का इतिहास अभिव्यक्त होता है और जिसे हर भारतीय पड़ना पसंद करेगा।
क्रांतिकारियों के सिर्फ इतने ही मुकदमे नहीं हैं। इनके अतिरिक्त और कितने ही मुकदमे हैं, लेकिन इन कुछ मुकदमों को चुनने का कारण यह था कि वे भारत के स्वाधीनता-संग्राम का क्रमबद्ध इतिहास बताते हैं।
बहादुरशाह ज़फर का मुकदमा ऐतिहासिक लाल किले के भीतर चलाया गया पहला मुकदमा था, जिसमें एक सम्राट पर एक साधारण व्यक्ति की तरह राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायविधि के नियम-कानून का पूर्णतः उल्लंघन किया गया। एक सम्राट को न तो कोई सम्मान दिया गया, न प्रतिवाद के लिए न्यायिक सहयोग ही। सारे गवाह भी अंग्रेजी हुकूमत के ताबेदार थे। मुगल साम्राज्य का सूरज डूब रहा था। फिर भी, न्याय कैसे किया जाता था, यह दिखाने में इस मुकदमे की अपनी भूमिका है।
लोकमान्य गंगाधर तिलक को इस देश में कौन नहीं जानता। उन्हें ‘भारतीय स्वाधीनता संग्राम का पितामह’ कहा गया है, क्योंकि वही महात्मा गांधी को राजनीतिक रणभूमि में लाये थे। तिलक एक विद्वान, पत्रकार तथा लेखक थे, जो बराबर ब्रिटिश कुशासन, शोषण और पक्षपात के विरुद्ध लिखते रहे। इन उत्तेजक लेखों के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। तिलक ने अपना बचावनामा खुद लिखा और निडर होकर कहा : ‘आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।’ अदालत में कहा गया यह अंतिम वाक्य अमर हो चुका है और आज भी बंबई उच्च न्यायलय की इमारत के केंद्रीय कक्ष में अंकित है।
‘बंगाल का शेर’ कहलाने वाले सुरेन्द्रनाथ बनर्जी पर मुकदमा चालाया गया, जब उन्होंने एक अंग्रेज न्यायाधीश की आलोचना करने का साहस किया। उन्हें कारावास का दंड दिया गया, जिसका उन्होंने यह कहकर स्वागत किया कि ‘मुझे अपनी पीढ़ी और अपने रुतबे के पहले ऐसे भारतीय होने का गौरव मिला था, जिसे जन-कर्तव्य पालन के लिए कारावास का दंड झेलना पड़ा।’
अलीपुर बम-कांड में श्री अरविंद घोष का मुकदमा ऐसा राजकीय मुकदमा था, जिसमें अभियुक्त पर एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश अफसर के कत्ल की कोशिश करने, चूकने और दूसरे को मार बैठने का आरोप लगाया गया था। कालांतर में यह अभियुक्त भारत के प्रमुख संत, पैगंबर और आध्यात्मिक नेता बने, जबकि उनके बचाव वकील सी.आर. दास एक स्वाधीनता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध हुए। सी.आर. दास का बचाव-वक्तव्य बार-बार पढ़े जाने योग्य है। मैंने मुकदमे को मूल रूप में पढ़कर यही महसूस किया कि एक छोटे-से लेख में उनके प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करना काफी मुश्किल काम है। यह मुकदमा दो महान व्यक्तियों के उत्थान का कारण बना। पहले ने आध्यात्मिक संस्कृति को समृद्ध बनाया, तो दूसरे ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को ऊर्जा प्रदान की।
‘वीर सावरकर’ के नाम से प्रसिद्ध विनायक दामोदर सावरकर बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने विदेश में पढ़ते वक्त क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। उनकी गिरफ्तारी, निर्वासन, उनका फरार होना, तथा फ्रांसिसी पुलिस द्वारा पुनः बंदी बनाया जाना—एक नाटकीय कथा की तरह है। उनके मुकदमे तो इससे भी बढ़कर हैं। उन पर भारत में भी मुकदमा चलाया गया और ‘द हेग’ के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ निर्णय न्यायालय में भी, जिससे विदेशी शासन से मुक्ति की भारतीय आकांक्षाओं से सारा विश्व परिचित हुआ। इस मुकदमें में यह भी दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ निर्णय न्यायालय में अपने हक में फैसला कराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस तरह अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल किया।
महात्मा गांधी के ‘यंग इंडिया’ में प्रकाशित विवादास्पद लेखों के कारण उन पर और प्रकाशक शंकरलाल बेंकर पर चलाया गया मुकदमा न्यायाधीश की निष्पक्षता और सौजन्यता के कारण विश्व के न्यायिक इतिहास के आलेख में दर्ज है। मुख्य न्यायाधीश जे.एम. शेलेट ने लिखा है : ‘‘सुकरात के मुकदमे को छोड़कर पूरे मानव इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मुकदमा होगा, जिसने गांधीजी के मुकदमे की तरह इतना तहलका मचाया हो और मानव-जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाला हो। नियमों पर सत्य की विजय की यह एक मिसाल है। न्याय का सम्मान होना चाहिए, और एक न्यायाधीश को अपना फर्ज निभाना चाहिए।’’ मुकदमे के मुख्य न्यायाधीश के कथन भी उद्धत करने योग्य हैं : ‘‘मेरा मानना यह है कि आपको तिलक महोदय की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, अर्थात् हर अभियोग पर दो साल साधारण कारावास, कुल मिलाकर 6 साल। यही दंड आपको देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। लेकिन ऐसा करते वक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर भावी परिस्थितियों में सरकार आपकी सजा घटाने या आपको रिहा करने का निर्णय लेती है, तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी।’’
स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में सरदार भगत सिंह के मुकदमे का अपना विशिष्ट स्थान है। भगत सिंह और उसके साथियों द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने, सांडर्स नामक ब्रिटिश अफसर को मारने और फिर मुकदमे का सामना करने के साहसपूर्ण कार्य से स्वाधीनता संग्राम को एक नया आवेग मिला था। भगत सिंह ने अपने किये को न्यायोचित ठहराते हुए अपना बचावनामा खुद लिखा था, जिसे उनके वकील आसफ अली ने पढ़कर सुनाया था। वक्तव्य में कहा गया था : ‘‘इंग्लैंड को उसकी स्वप्न-निद्रा से जगाने के लिए बम फेंकना जरूरी था। असेंबली के बीच बम फेंककर हमने उन लोगों की तरफ से विरोध प्रकट किया, जिनके पास अपनी हार्दिक वेदना को व्यक्त करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारा एक मात्र उद्देश्य बहरों को सुनाना और असावधानों को वक्त रहते चेतावनी देना था।’’
लेबर पार्टी की हुकूमत के वक्त चलाया गया यह मुकदमा इस बात का प्रमाण है कि अंग्रेजी नीति ही आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन की थी, सरकार भले ही ‘लेबर’ की हो या ‘कंजरवेटिव्स’ की। इतना ही नहीं, भारत में ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था का एक ही उद्देश्य था—अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने वालों का दमन करना।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उभरती कुछ प्रवृत्तियों और कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती गतिविधियों को देखकर भी ब्रटिश शासन को काफी चिंता थी। बुद्धिजीवियों की एक बड़ी संख्या वाली कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा तथा श्रमिक वर्ग तक पहुंच गयी थी। फिर, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से भी खतरा था क्योंकि भारतीय कम्युनिस्टों का उससे गहरा संबंध था। उनकी विचार धारा भी वहीं से ली गयी थी। इसलिए कई प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया गया और ब्रिटिश प्रभुसत्ता के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। कायदे से मुकदमा वहीं चलाया जाना चाहिए था जहां जूरी उनका परीक्षण कर सके, लेकिन जूरी से बचने के लिए मुकदमे को मनमाने ढंग से उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थानांतरित कर दिया गया। अदालत ने जानबूझकर एक ऐसी विवादास्पद कार्यविधि का पालन किया, जिससे अभियुक्तों को दोषी ठहराया जा सके। यह मुकदमा चार साल तक खिंचा। सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारपत्रों में उसे छापा गया और ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था का हास्यास्पद चरित्र उजागर हो गया। श्रमिक वर्ग को संगठित करने में इस मुकदमे से बहुत सहायता मिली।
महान बुद्धिजीवी और क्रांतिकारी एम.एन. राय ‘कम्युनिस्ट इंटरनेशनल’ के संस्थापकों में एक थे। रूसी क्रांति के समय लेनिन के साथ काम करने वाले वह एकमात्र भारतीय थे। भारत के क्रांतिकारियों और उनकी गतिविधियों को एम.एन. राय का समर्थन मिलना ब्रिटिश सरकार के लिए गंभीर खतरा था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमे के समय वह विदेश में थे। सन् 1931 में भारत लौटने पर उन्हें नाटकीय परिस्थितियों में षड्यंत्र और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राय ने अपना बचावनामा खुद लिखा, जिसे उनके वकील ने पढ़कर सुनाया। यह बचावनामा एक साधारण शोध-प्रबंध है—शोषित, दीन-दुखियों के अधिकारों की प्रतिरक्षा करता हुआ, उन्हें अपनी गरीबी हटाने, शोषकों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता हुआ। एम.एन. राय ने भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का इतिहास कुरेदते हुए लिखा-‘‘सत्ता हथियाने वाली ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी लड़ाई का रास्ता ही भारत में संवैधानिक सरकार की स्थापना का एकमात्र रास्ता है।’’ बचाव की यह दलील सर्वाधिक न्यायोचित, तार्किक और सुसंगत दस्तावेजों में से एक है। भले ही उनके अपने बचाव में इसका इस्तेमाल न हो सका, लेकिन आजाद हिंद फौज (आई.एन.ए.) पर शेख अब्दुल्ला के मुकदमों की प्रतिवादी दलील तैयार करने में क्रमशः भूलाभाई देसाई और आसफ अली को इससे आधार और प्रेरणा मिली।
सन् 1945 में आजाद हिंद फौज के तीन अफसरों का मुकदमा ब्रिटिश सरकार के शक्ति-प्रदर्शन का अंतिम प्रयास था। जनमहत्व के मूलभूत मुद्दों को जोड़ते हुए सुप्रतिष्ठित वकीलों का एक दल भारतीय अफसरों के बचाव के लिए सामने आया। ‘हर राष्ट्र को अपनी आजादी के लिए लड़ने का अधिकार है’-यह तर्क ब्रिटिश सेना के विरुद्ध आजाद हिंद फौज के गठन को न्यायोचित ठहराता था। इस मुकदमें में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के व्यापक और नवीन पक्षों पर बहस हुई। देश को आजाद कराने की नेताजी की यह साहसपूर्ण कोशिश इतिहास में अपूर्व तो थी ही, हर भारतीय के लिए अद्भुत, आकर्षक और प्रेरणादायक भी थी। इस मुकदमे से भारत में ब्रटिश शासन का अंत हुआ।
इतिहास को पूरा करने के लिए शेख अब्दुल्ला के मुकदमे को भी इससे जोड़ दिया गया है। अंग्रेज देशी प्रांत में प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन शाही रियायतों में नवाबों के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन करते थे। देशी रियासतों के शासक अपनी प्रजा की जिंदगी, आजादी और संपत्ति पर असीमित निरंकुश सत्ता रखते थे। पराधीन भारत की कई देशी रियासतों में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए समानांतर आंदोलन हुए। देशी राजाओं ने इन आंदोलनों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कश्मीर के एक महत्वपूर्ण नेता शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के निरंकुश शासन के विरुद्ध कश्मीरियों को संगठित किया। सन् 1946 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, ये शासक अपनी रियासतें छोड़ने को तैयार न थे। शेख अब्दुल्ला ने महाराजा को गद्दी से हटाने के लिए कश्मीरवासियों का आह्वान किया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया।
सुप्रसिद्ध भारतीय वकील आसफ अली ने अन्य योग्य वकीलों के साथ मिलकर अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ा। हालांकि शेख अब्दुल्ला को दोषी ठहराया गया, लेकिन यह मुकदमा उनके लिए नैतिक विजय साबित हुआ और 1947 में वह कश्मीर के पहले ‘प्रिमीयर’ बने।
जिस तरह आजाद हिंद फौज मुकदमा भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करने वाला मुकदमा था, उसी तरह शेख अब्दुल्ला का मुकदमा देशी रियासतों में नवाबों के निरंकुश शासन का अंत कर पूर्ण स्वराज्य लाने का मुकदमा था।
ये मुकदमे एक तरह से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के 90 वर्षों के इतिहास की कथा कहते हैं। पाठकों को इनसे उन साहसी स्वतंत्रता-सेनानियों के चरित्र को समझने की गहरी अंतर्दृष्टि मिलेगी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हर चुनौती का सामना किया तथा अपना सर्वस्व त्याग दिया।
बहादुरशाह ज़फर
(1775-1862)
दिल्ली के शासक अकबर द्वितीय के पुत्र अबू
ज़फर, बाबर द्वारा सन् 1526 में
स्थापित मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। सन् 1837 में राजगद्दी पर बैठने
के बाद उन्हें अबू ज़फर मुहम्मद सराजुद्दीन बहादुरशाह गाजी का खिताब मिला
था। ‘ज़फर’ शायर के रूप में उनका उपनाम था।
अबू ज़फर के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म कहाँ हुआ, इस पर भी रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। उन्हें उर्दू, अरबी और फारसी के परम्परागत शिक्षा मिली, तो घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और बंदूक चलाने की सैनिक शिक्षा भी मिली। इन कलाओं में उन्होंने काफी महारात हासिल की। वह सूफी दर्शन के अध्येता, फारसी के विद्वान, सुलेखन में दक्ष और शायर थे। उनके गुरु के दो महान शायर इब्राहिम ज़ौक और असद उल्ला खां ग़ालिब शायरी में उनके गुरु थे। निर्वासन के समय ज़फर ने जो गजलें लिखीं, वे अपनी संगीतात्मकता और संवेदना के लिए साहित्य में अपनी खास जगह रखती हैं। उन्हें शराब या तंबाकू का शौक न था, लेकिन अच्छे खाने के वे बड़े शौकीन थे।
उन्होंने कई विवाह किये और उनके पास बेगमों, दासियों और रखैलों को पूरा हरम था। उनकी सबसे पसंदीदा बेगम जीनत महल थीं, जिनसे उन्होंने उम्र ढलने पर विवाह किया था और जो निर्वासन ओर बदकिस्मती के अंतिम दिनों में उनके साथ थीं।
एक शासक के रूप में बहादुरशाह हिंदुस्तान के अंग्रेजों को कानूनन अपनी प्रजा समझते थे, क्योंकि 1765 में उनके दादा शाह आलम ने बंगाल की जिस दीवानी पर हस्ताक्षर किये थे, उसकी शर्तों के तहत अंग्रेजों ने स्वामिभक्ति की शपथ ली थी। यह अलग बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार उन्हें सिर्फ एक पेंशनभोगी और नाममात्र का शासक समझती थी, जो हर माह एक लाख रुपए के वजीफे का हकदार था और जिसका अधिकार-क्षेत्र लाल किले की चारदीवारी तक सीमित था।
सन् 1857 के विद्रोह के समय बहादुरशाह 82 वर्ष के थे। 11 मई 1857 को मेरठ से आये विद्रोही सिपाही और अफसर किले में घुस गये और उन्होंने बादशाह से सहायता और संरक्षण की मांग की। न चाहते हुए भी बहादुरशाह को उनकी मदद करनी पड़ी। हां, उन्होंने यह जरूर कहा कि अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए उनके पास न तो साधन हैं, न खजाना, और न ही रसद। आगे के संघर्षमय दिनों में उनका कोई खास योगदान न था। सितंबर के अंत में विद्रोहियों के दिल्ली हार जाने के बाद बहादुरशाह हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गये। बाद में अंग्रेजों द्वारा जान बख्श देने के वायदे पर उन्होंने समर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने राजद्रोह, षड्यंत्र, विद्रोह और कत्ल के आरोप में सैनिक अदालत द्वारा उन पर मुकदमा चलाया। मुकदमे में पेश किये गये सबूत अधिकांशतः अप्रासंगिक और कानूनन अमान्य थे, लेकिन बहादुरशाह को सभी आरोपों में दोषी पाया गया और रंगून निष्कासित कर दिया गया।
कुछ भारतीय इतिहासकारों ने सन् 1857 के विद्रोह में बहादुरशाह की भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर लिखा है, लेकिन अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ाई में एक बादशाह और एक जनांदोलन के नेता की प्रभावपूर्ण भूमिका निभाना उनके लिए संभव न था। वह बहुत कमजोर, अनभिज्ञ, युद्धकला में अनुभवहीन और साधकहीन शासक थे। उनका मुकदमा और निष्कासन स्पष्टतः न्याय का उपहास था और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित था।
अबू ज़फर के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म कहाँ हुआ, इस पर भी रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। उन्हें उर्दू, अरबी और फारसी के परम्परागत शिक्षा मिली, तो घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और बंदूक चलाने की सैनिक शिक्षा भी मिली। इन कलाओं में उन्होंने काफी महारात हासिल की। वह सूफी दर्शन के अध्येता, फारसी के विद्वान, सुलेखन में दक्ष और शायर थे। उनके गुरु के दो महान शायर इब्राहिम ज़ौक और असद उल्ला खां ग़ालिब शायरी में उनके गुरु थे। निर्वासन के समय ज़फर ने जो गजलें लिखीं, वे अपनी संगीतात्मकता और संवेदना के लिए साहित्य में अपनी खास जगह रखती हैं। उन्हें शराब या तंबाकू का शौक न था, लेकिन अच्छे खाने के वे बड़े शौकीन थे।
उन्होंने कई विवाह किये और उनके पास बेगमों, दासियों और रखैलों को पूरा हरम था। उनकी सबसे पसंदीदा बेगम जीनत महल थीं, जिनसे उन्होंने उम्र ढलने पर विवाह किया था और जो निर्वासन ओर बदकिस्मती के अंतिम दिनों में उनके साथ थीं।
एक शासक के रूप में बहादुरशाह हिंदुस्तान के अंग्रेजों को कानूनन अपनी प्रजा समझते थे, क्योंकि 1765 में उनके दादा शाह आलम ने बंगाल की जिस दीवानी पर हस्ताक्षर किये थे, उसकी शर्तों के तहत अंग्रेजों ने स्वामिभक्ति की शपथ ली थी। यह अलग बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार उन्हें सिर्फ एक पेंशनभोगी और नाममात्र का शासक समझती थी, जो हर माह एक लाख रुपए के वजीफे का हकदार था और जिसका अधिकार-क्षेत्र लाल किले की चारदीवारी तक सीमित था।
सन् 1857 के विद्रोह के समय बहादुरशाह 82 वर्ष के थे। 11 मई 1857 को मेरठ से आये विद्रोही सिपाही और अफसर किले में घुस गये और उन्होंने बादशाह से सहायता और संरक्षण की मांग की। न चाहते हुए भी बहादुरशाह को उनकी मदद करनी पड़ी। हां, उन्होंने यह जरूर कहा कि अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए उनके पास न तो साधन हैं, न खजाना, और न ही रसद। आगे के संघर्षमय दिनों में उनका कोई खास योगदान न था। सितंबर के अंत में विद्रोहियों के दिल्ली हार जाने के बाद बहादुरशाह हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गये। बाद में अंग्रेजों द्वारा जान बख्श देने के वायदे पर उन्होंने समर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने राजद्रोह, षड्यंत्र, विद्रोह और कत्ल के आरोप में सैनिक अदालत द्वारा उन पर मुकदमा चलाया। मुकदमे में पेश किये गये सबूत अधिकांशतः अप्रासंगिक और कानूनन अमान्य थे, लेकिन बहादुरशाह को सभी आरोपों में दोषी पाया गया और रंगून निष्कासित कर दिया गया।
कुछ भारतीय इतिहासकारों ने सन् 1857 के विद्रोह में बहादुरशाह की भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर लिखा है, लेकिन अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ाई में एक बादशाह और एक जनांदोलन के नेता की प्रभावपूर्ण भूमिका निभाना उनके लिए संभव न था। वह बहुत कमजोर, अनभिज्ञ, युद्धकला में अनुभवहीन और साधकहीन शासक थे। उनका मुकदमा और निष्कासन स्पष्टतः न्याय का उपहास था और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i