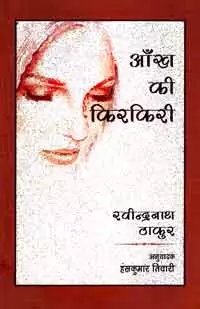|
पारिवारिक >> कुलवधू कुलवधूरबीन्द्रनाथ टैगोर
|
365 पाठक हैं |
|||||||
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार की दिल की गहराइयों को छूने वाली कृति....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
उस मासूम की जागती आंखों में शादी के बाद के ढेरों सपने थे। हर लड़की
देखती हैं, ऐसे सपने। उसकी डोली उठी भी। वह बनी चंद्रद्वीप राजवंश की
‘कुलवधू’। लेकिन उसके सारे सपने तार-तार हो बिखर गए।
उसका पति उसके सपनों का राजकुमार नहीं था। वह तो था झूठे
‘अहम्‘ में मस्त एक महाराजा। उसके अहंकार से टकरा कर
‘कुलवधू’ की सारी खुशियों ने दम तोड़ दिया।
‘कुलवधू’ की ऐसी दशा के लिए कौन था जिम्मेदार ? क्या सिर्फ उसका पति ही या फिर उसका पिता भी ? पति और पिता के अहम् के चट्टानों के बीच पिसती पत्नी और बेटी की ह्रदयस्पर्शी कथा है कुलवधू।
‘कुलवधू’ की ऐसी दशा के लिए कौन था जिम्मेदार ? क्या सिर्फ उसका पति ही या फिर उसका पिता भी ? पति और पिता के अहम् के चट्टानों के बीच पिसती पत्नी और बेटी की ह्रदयस्पर्शी कथा है कुलवधू।
1861-1941
सन् 1861, 7 मई को कलकत्ता (कोलकाता) में जन्मे कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर को उनकी श्रेष्ठ कृति गीतांजलि पर ‘नोबल पुरस्कार’ सन् 1913 को प्रदान किया गया था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी टैगोर (ठाकुर) की लेखनी ने कथा, कविता के साथ ही उपन्यास की विधा में कमाल दिखाया। संवेदनशील हृदय, अतींद्रिय अस्मिता को देखने वाली प्रज्ञा और सामाजिक संदर्भों में भारतीय मूल्यों के प्रति निष्ठा का भाव उनकी प्रत्येक कृति में स्पष्ट झलकता है। धरती की सोंधी खुशबू को महसूस करते हुए उनकी कल्पना सहज ही आकाश की अनंत-असीम ऊंचाइयों को छूने के लिए उड़ती चली जाती है। उनकी यही खासियत उन्हें जहाँ एक आम आदमी से जोड़ती है, वहीं उस दिव्यता का संस्पर्श भी कराती है, जो उसमें बैठा लौकिक दिखता हुआ भी वास्तव में अलौकिक है।
प्रस्तुत है उनकी लेखनी के चमत्कार की एक झलक ‘बहूरानी का हाट’ नामक बंगला उपन्यास का हिंदी रूपांतर ‘कुलवधू’- रिश्तों के बीच अपने अस्तित्व को ढूँढ़ती एक नारी की हृदयस्पर्शी गाथा।
विभा उदयादित्य के पांवों में पड़कर रोने लगी। उदयादित्य के भी आंसू गिरने लगे। विभा के सिर पर हाथ रखकर वे बोले- ‘‘तू क्यों रोती है भला ! यहां कौन-सा सुख था तुझे, चारों ओर केवल दुख, कष्ट और शोक-ही-शोक। इस कारागार से मुक्त हो तुम बच गईं।’’
राममोहन की आंखों में आंसू भर आए, वह बोला-‘‘यह क्या बेवकूफी कर रही हो मां लक्ष्मी, तुम हंसती-मुस्कराती अपने घर चलो। आज के शुभ दिन आंसू न बहाओ, आंखों को पोंछ डालो।’’’
सन् 1861, 7 मई को कलकत्ता (कोलकाता) में जन्मे कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर को उनकी श्रेष्ठ कृति गीतांजलि पर ‘नोबल पुरस्कार’ सन् 1913 को प्रदान किया गया था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी टैगोर (ठाकुर) की लेखनी ने कथा, कविता के साथ ही उपन्यास की विधा में कमाल दिखाया। संवेदनशील हृदय, अतींद्रिय अस्मिता को देखने वाली प्रज्ञा और सामाजिक संदर्भों में भारतीय मूल्यों के प्रति निष्ठा का भाव उनकी प्रत्येक कृति में स्पष्ट झलकता है। धरती की सोंधी खुशबू को महसूस करते हुए उनकी कल्पना सहज ही आकाश की अनंत-असीम ऊंचाइयों को छूने के लिए उड़ती चली जाती है। उनकी यही खासियत उन्हें जहाँ एक आम आदमी से जोड़ती है, वहीं उस दिव्यता का संस्पर्श भी कराती है, जो उसमें बैठा लौकिक दिखता हुआ भी वास्तव में अलौकिक है।
प्रस्तुत है उनकी लेखनी के चमत्कार की एक झलक ‘बहूरानी का हाट’ नामक बंगला उपन्यास का हिंदी रूपांतर ‘कुलवधू’- रिश्तों के बीच अपने अस्तित्व को ढूँढ़ती एक नारी की हृदयस्पर्शी गाथा।
विभा उदयादित्य के पांवों में पड़कर रोने लगी। उदयादित्य के भी आंसू गिरने लगे। विभा के सिर पर हाथ रखकर वे बोले- ‘‘तू क्यों रोती है भला ! यहां कौन-सा सुख था तुझे, चारों ओर केवल दुख, कष्ट और शोक-ही-शोक। इस कारागार से मुक्त हो तुम बच गईं।’’
राममोहन की आंखों में आंसू भर आए, वह बोला-‘‘यह क्या बेवकूफी कर रही हो मां लक्ष्मी, तुम हंसती-मुस्कराती अपने घर चलो। आज के शुभ दिन आंसू न बहाओ, आंखों को पोंछ डालो।’’’
कुलवधू
रात बहुत बीच चुकी है। गरमी का मौसम है। हवा बिल्कुल बंद है। पेड़ के
पत्ते तक नहीं हिल रहे। यशोहर के युवराज, प्रतापादित्य के जेष्ठ पुत्र
उदयादित्य अपने शयनकक्ष के झरोखे से लगे बैठे हैं। उनके समीप बैठी है उनकी
पत्नी सुरमा।
सुरमा ने कहा-‘‘प्रियतम, सब सहते रहो, धीरज रखो कभी-न-कभी तो सुख के दिन आएँगे ही।’’‘‘ मैं और कोई सुख नहीं चाहता।’’ उदयादित्य ने कहा-‘‘मैं तो यही चाहता हूं कि मैं राजप्रसाद में न जन्मा होता, युवराज न होता, यशोहर-अधिपति की क्षुद्रतम, तुच्छतम प्रजा की भी प्रजा होता, उनका ज्येष्ठ पुत्र-उनके सिंहासन, उनके समस्त धन, मान और यश-गौरव का एकमात्र उत्तराधिकारी न होता। कौन-सी तपस्या करूं जिससे यह समस्त अतीत उलटा जा सके।’’
सुरमा ने अत्यंत कातर होकर युवराज का दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उनके चेहरे की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। युवराज की मनोभिलाषा पूरी करने के लिए वह अपने प्राण भी दे सकती है, लेकिन दुख तो यही है कि प्राण देकर भी युवराज की इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता।
युवराज ने फिर कहा-‘‘सुरमा, राजा के घर जन्म लेने के कारण ही मैं सुखी न हो पाया। राजा के घर शायद उत्तराधिकारी ही जन्म लेते हैं, संतान के रूप में कोई जन्म नहीं लेता। पिता बचपन से ही प्रतिक्षण मेरी परीक्षा लेते आ रहे हैं कि मैं उनके द्वारा उपार्जित यशमान की रक्षा कर सकूंगा या नहीं, वंश का मुख उज्ज्वल कर सकूंगा या नहीं राज्य के भारी उत्तरदायित्व को संभाल सकूंगा या नहीं। उन्होंने मेरे प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक चेष्टा को परीक्षा की दृष्टि से देखा है, स्नेह की दृष्टि से नहीं। आत्मीयजन, मंत्री, राजसभासद और प्रजागण सभी मेरे प्रत्येक कार्य और मेरी प्रत्येक बात को कसौटी पर कस-कसकर मेरे भविष्य का आकलन करते रहे हैं। सबके सब सिर हिलाकर कहते हैं-उहूं, इस संकट में मैं राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं समझ पाता। सब मेरी अवहेलना करने लगे। पिताजी मुझसे घृणा करने लगे। यहां तक कि मुझसे उन्हें कोई आशा ही नहीं रह गई। मेरी खोज-खबर तक नहीं लेते।’’
सुरमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा-‘‘हाय, उनसे रहा कैसे जाता है ?’’
उसे दुख हुआ, उसे गुस्सा आया, ‘जो तुम्हें अबोध समझते हैं, वे स्वयं ही अबोध हैं।’
उदयादित्य धीरे से मुस्कराए। सुरमा की ठोड़ी पकड़कर उन्होंने गुस्से से लाल हो आए उसके मुखड़े को थपथपा दिया। दूसरे ही क्षण गम्भीर होकर बोले-‘‘नहीं सुरमा, राजकाज चलाने की बुद्धि सचमुच मुझमें नहीं। यह सिद्ध हो चुका है। जब मैं सोलह वर्ष का था, शासन-प्रबंध की शिक्षा देने के लिए महाराज ने हुसेनखाली परगने का भार मुझे सौंपा था। छः महीने में ही बड़ी गड़बड़ी शुरू हो गई। राजस्व घटने लगा, लेकिन प्रजा आशीर्वाद देने लगी। राज-कर्मचारी मेरे विरुद्ध महाराज से शिकायतें करने लगे। राजसभा के सभी सदस्यों की एक ही राय स्थापित हो गई कि युवराज चूंकि प्रजा के इतने प्रिय-पात्र हो गए हैं, इसलिए अब वे राज का शासन किसी भी प्रकार नहीं कर सकते। उस दिन से महाराज मेरी ओर देखते तक नहीं। वे कहते रहे, यह कुलांगार रायगढ़ के बूढ़े बसंतराय के समान ही होगा, सितार बजाकर नाचता फिरेगा और सारे राज्य को चौपट करके रख देगा।’’
सुरमा ने फिर कहा-‘‘प्रियतम, थोड़ा धीरज रखो। आखिर वे आपके पिता हैं। इस समय राज्य-उपार्जन और राज्य वृद्धि की एकमात्र दुराशा से उनका हृदय विचलित है, वहां स्नेह के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। जितनी दूर तक उनकी अभिलाषा पूरी होती रहेगी, उनके स्नेह के साम्राज्य में भी उतनी ही बढ़ोत्तरी होती रहेगी।’’
युवराज ने कहा-‘‘तुम्हारी बुद्धि तीव्र और दूरदर्शी है, सुरमा, किंतु इस बार तुम गलत समझ रही हो। एक तो अभिलाषा का कोई अंत नहीं, दूसरे पिताजी के राज्य की सीमा जितनी ही बढ़ती जाएगी उसके हाथ से निकल जाने का उनका भय भी उतना ही बढ़ता जाएगा और मुझे वे उतना ही अधिक उसके अनुपयुक्त समझते जाएंगे।’’
सुरमा ने गलत नहीं समझा था, केवल गलत विश्वास किया करती थी और विश्वास बुद्धि को भी लांघ जाता है। वह संपूर्ण मन से चाहती रही कि ऐसा ही हो।
उदयादित्य बिना रुके कहते गए-‘‘चारों ओर कहीं कृपादृष्टि और कहीं अवहेलना सहन न कर पाता तो मैं बीच-बीच में भागकर राजगढ़ दादा साहब के पास चला जाता था। पिताजी तो कभी खोज-खबर लेते नहीं थे। ओह, वहां जाते ही कैसा परिवर्तन हो जाता था। वहां पेड़-पौधे और बाग-बगीचे देखने को मिलते, ग्रामीणों के झोंपड़ों में जा सकता था। दिन-रात राजवेश धारण किए नहीं रहना पड़ता था। इसके अलावा जहां दादा साहब रहते हैं, वहां विषाद, चिंता और कठोर गांभीर्य फटने भी नहीं पाता था। वे गा-बजाकर, आमोद-प्रमोद कर चारों दिशाओं को गुंजायमान किए रहते थे। उनके चारों ओर प्रसन्नता, शांति और सद्भावना विराजती थी। वहां जाकर मैं भूल जाता कि मैं यशोहर का युवराज हूं। कितनी सुखद भूल होती थी वह ! और एक दिन जब मेरी उम्र अट्ठारह वर्ष की रही होगी, रायगढ़ में तब बसंती हवा चल रही थी, तभी एक सघन निकुंज में मैंने रुक्मिणी को देखा...।’’
सुरमा बोल उठी-‘‘यह बात तो मैं कई बार सुन चुकी हूं।’’
उदयादित्य ने कहा-‘‘और एक बार सुन लो। रह-रहकर उस समय की एक-एक बात हृदय को कचोटती रहती है। यदि कहकर इसे बाहर न निकाल दूं तो भी प्राण बचेंगे कैसे ! और यह बात तुम्हें बताते हुए अब भी संकोच और कष्ट का अनुभव होता है, इसी से बार-बार कहा करता हूं, जिस दिन कहने में संकोच और कष्ट न होगा, उस दिन समझ लूंगा कि मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ, और तब उसकी चर्चा कभी नहीं करूंगा।’’
सुरमा ने कहा-‘‘प्रायश्चित किस बात का, प्रियतम ? यदि तुमने पाप भी किया हो तो वह पाप का दोष है, तुम्हारा दोष नहीं। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती ? क्या अन्तर्यामी तुम्हारे मन को देख नहीं पाते ?’’
उदयादित्य ने सुरमा की बात अनसुनी करके कहा-‘‘रुक्मिणी मुझसे उम्र में तीन वर्ष बड़ी थी। बेचारी, अकेली और विधवा। दादा साहब के अनुग्रह के कारण वह किसी तरह रायगढ़ में टिक पाई थी। नहीं जानता कि किस कौशल से उसने मुझे अपनी ओर पहली बार में ही आकर्षित कर लिया था। उस समय मेरे मन में दोपहर की धूप खिल रही थी। इतना प्रखर आलोक था कि मैं कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। चारों ओर सृष्टि ज्योतिर्मय भाप से आच्छादित प्रतीत होती थी। शरीर का समस्त रक्त मानो सिर पर चढ़ गया था, कुछ भी विचित्र और असंभव नहीं लगता था, पथ-कुपथ, दिशा-अदिशा सब कुछ एकाकार प्रतीत होते थे। उससे पूर्व कभी मेरी ऐसी दशा नहीं हुई, उसके बाद भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। जगदीश्वर ही जानें, उन्होंने अपने किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस क्षुद्र, दुर्बल हृदय के विरुद्ध, एक दिन के लिए समस्त जगत को इस प्रकार उत्तेजित कर दिया कि सचराचर सृष्टि एकतंत्र होकर इस हृदय को क्षण में विपथ की ओर बहा ले गई। अधिक नहीं, केवल क्षण भर के लिए समस्त बहिर्जगत का एक क्षण स्थायी और दारुण आघात लगा और उसी क्षण में यह दुर्बल हृदय जड़ से उखड़ गया-विद्युत-वेग से वह धूल में जा गिरा। उसके बाद जब वह उठा तो धूल-धूसरित और म्लान था-वह धूल फिर पुछ नहीं सकी, उस मलिनता का चिन्ह फिर नहीं मिटा। मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया था कि विधाता ने एक क्षण में मेरे जीवन की समस्त उज्ज्वलता को काला कर दिया ? दिन को रात में परिवर्तित कर दिया। मेरे हृदय के पुष्पोद्यान में खिल रहे मालती और जूही के विहंसते मुखड़े भी ग्लानि से मलिन पड़ गए।’’
कहते-कहते उदयादित्य का गोरा चेहरा आरक्त हो उठा, आंखें फैल गईं, सिर से लेकर पांवों तक बिजली-सी कौंध गई जैसे।
सुरमा ने हर्ष, गर्व और कष्ट से सिहरकर कहा-‘‘ अब इसे रहने भी दो, तुम्हें मेरे सिर की सौगंध !’’
लेकिन उदयादित्य कहते ही गए-‘‘धीरे-धीरे रक्त की उष्णता शांत हुई और तब मैं सारी वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखने लगा। जब विश्व विक्षुब्ध और बौखलाए, डोलते-डगमगाते और सुर्ख आंखों वाले किसी पागल के दिमाग में चक्करघिन्नी खाती हवाई सनक की तरह नहीं बल्कि स्वाभाविक कार्यक्षेत्र के रूप में दिखाई देने लगा तो मन की न जाने कैसी अवस्था हो गई थी। तब पहली बार पता चला कि कहां आ गिरा हूं। हजारों-लाखों कोस नीचे पाताल के गहन गह्वर में, अंधतम रजनी के बीच पलक झपकते ही आ गिरा हूं। तब दादा साहब स्नेहपूर्वक बुला ले गए। भला मैं उनको अपना मुंह दिखा ही कैसे पाया। लेकिन उसी समय मुझे रायगढ़ छोड़ देना पड़ा। दादा साहब मुझे देखे बिना रह नहीं सकते थे। वे मुझे बराबर बुलावा भेजते। परंतु मेरे मन में ऐसा डर समा गया था कि जाते नहीं बना। तब वे स्वयं मुझे बहन विभा को देखने के लिए आने लगे। कोई अभिमान नहीं, कोई उलाहना नहीं। इतना भी नहीं पूछते कि मैं क्यों नहीं जाता। हमसे मिलते, हंसी-खुशी मनाते और लौट जाते।’’
उदयादित्य ने किंचित् मुस्कराकर अतिशय मृदुल कोमल प्रेम से अपने बड़े-बड़े तरल नेत्रों से सुरमा की ओर देखा। सुरमा समझ गई कि इस बार कौन-सी बात छिड़ने वाली है। उसका चेहरा झुक गया, वह कुछ चंचल हो उठी। युवराज ने दोनों हाथों से सुरमा के कपोलों को पकड़कर चेहरे को ऊपर उठाया फिर उससे सटकर बैठ गए और धीरे से उसके मुख-मंडल को अपने कंधे पर रख लिया। बाएं हाथ से उसकी कमर को पकड़ते हुए, गंभीर, प्रशांत, प्रेम से गाल को चूमकर उन्होंने कहा-‘‘उसके बाद क्या हुआ, बताओ तो सुरमा ? तुम्हारा यह बुद्धि से दीप्त, स्नेह-प्रेम से कोमल, हास्योज्ज्वल, प्रशांतभाव से विमल मुखड़ा, कहां से उदित हुआ ? मेरे मन में उस घनान्धकार के दूर होने की क्या कोई आशा थी ? तुम मेरी ऊषा हो, मेरा प्रकाश, मेरी आशा ! किस माया-मंत्र से तुमने उस अंधकार को मिटा दिया ?’’
युवराज बार-बार सुरमा का मुंह चूमने लगे। वह कुछ न बोली, आनंदातिरेक से उसकी आंखें भर आईं।
युवराज ने कहा-‘‘इतने दिनों के बाद मुझे सच्चा आश्रय मिला। तुम्हीं से प्रथम बार सुना कि मैं अबोध नहीं। उस पर विश्वास किया और स्वयं को वैसा ही समझने लगा। तुम्हीं से यह सीखा कि बुद्धि किसी अंधेरी संकरी गली के समान टेढ़ी-मेढ़ी और ऊंची-नीची नहीं, राजपथ की तरह सीधी, समतल और प्रशस्त होती है। पहले मैं अपने-आपसे घृणा करता था, स्वयं अपनी अवहेलना किया करता था। कोई काम करने का साहस नहीं कर पाता था। मन यदि कहता कि वह ठीक है तो आत्मसंशयी संस्कार कह उठता था कि शायद वह ठीक हो। जो जैसा व्यवहार करता था, सह लिया करता था। इतने दिनों के बाद समझ पाया कि मैं भी कुछ हूं। इतने दिनों तक मैं अदृश्य था जैसे तुमने मुझे बाहर निकाला। सुरमा, तुमने मेरा अविष्कार किया है। अब मेरा मन जिसे अच्छा कहता है, उचित समझता है, मैं उसे उसी क्षण करना चाहता हूं। तुम्हारे ऊपर मेरा इतना विश्वास है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मैं भी अपने-आप पर निर्भय होकर विश्वास कर पाता हूं। इस सुकोमल शरीर में इतनी शक्ति कहां छिपी थी, जिससे तुमने मुझे भी इतना शक्तिसंपन्न बना दिया ?’’
पूर्ण समर्पण के भाव से सुरमा पति के वक्षस्थल से लिपट गई। असीम उत्सर्गमयी दृष्टि से वह पति की ओर निहारती रही, मानो उसके नेत्र कह रहे हों, ‘मेरा और कोई नहीं, केवल तुम्हीं से मेरा सर्वस्व है।’
बचपन से उदयादित्य आत्मीयजनों की उपेक्षा सहते आए हैं, इसीलिए बीच-बीच में कभी-कभी निस्तब्ध गहन रात्रि में, सुरमा के समीप बैठकर सौ बार कही हुई उसी पुरानी जीवन-कथा को खंड-खंड कर कहना और फिर एक-एक बात की आलोचना करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है।
उदयादित्य ने कहा-‘‘इस तरह और कितने दिन चलेगा, सुरमा ! इधर राज्यसभा के सभासदगण एक प्रकार की दयाभरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हैं। उधर अंतःपुर में मां तुम्हें अपमानित करती रहती हैं। यहां तक कि दास-दासी भी तुम्हारा सम्मान नहीं करते। मैं किसी को अपनी बात बता नहीं पाता और चुपचाप सहता रहता हूं। तेजस्विनी होकर भी तुम चुपचाप सब कुछ सह लिया करती हो। मेरे कारण तुम्हें केवल अपमान और कष्ट ही सहना पड़ रहा है, इससे तो यही अच्छा था कि हमारा विवाह ही न होता।’’
सुरमा बोली-‘‘यह क्यों कहते हो, स्वामी ! ऐसे ही समय में तो तुम्हें सुरमा की आवश्यकता है। सुख के समय तो सुरमा विलास की वस्तु और क्रीड़ा की कठपुतली होती। समस्त दुखों का अतिक्रमण कर मेरे मन में यही सुख जाग रहा है कि मैं तुम्हारे काम आ रही हूं, तुम्हारे साथ दुख सहने में जो अतुल आनंद प्राप्त होता है, मैं उसी का उपभोग कर रही हूं। दुख केवल इस बात का है कि तुम्हारे समस्त कष्टों को मैं क्यों नहीं झेल पाती ?’’
युवराज कुछ देर चुप रहे, फिर बोले-‘‘दुख ? मुझे अपने लिए तो उतनी चिंता नहीं। अब सब कुछ सह्य हो गया है। दुख यही है कि मेरे लिए तुम्हें अपमान सहना पड़ता है, क्यों भला ? एक सच्ची नारी की भांति दुख में तुमने मुझे सांत्वना दी है, थक जाने पर विश्राम दिया है, लेकिन मैं एक पति की तरह तुम्हें अपमानित और लज्जित होने से नहीं बचा सका। तुम्हारे पिता श्रीपुरराज मेरे पिता को अपना अधिपति नहीं मानते, वे यशोहर की अधीनता स्वीकार नहीं करते, इसलिए मेरे पिता तुम्हारा निरादर कर अपने बड़प्पन को बनाए रखना चाहते हैं। अगर कोई तुम्हारा अपमान भी करे तो उस पर ध्यान नहीं देते। वे समझते हैं कि तुम्हें पुत्रवधू बनाया, यही बहुत ज्यादा हुआ, अब अधिक सहा नहीं जाता। कभी-कभी मन में आता है कि सब कुछ छोड़-छाड़कर तुम्हें लेकर कहीं अन्यत्र चला जाऊं। अब तक संभवतः चला भी जाता, केवल तुमने पकड़ रखा है।’’
रात बहुत बीत गई थी। संध्याकाल में उगने वाले कई तारे अस्त हो चुके थे। और गहन रात्रि में उगने वाले तारे चमक उठे थे। प्राकार-तोरण पर स्थित प्रहरियों की पदचाप दूर से ही सुनाई दे रही थी। सारा संसार गहरी निद्रा में लीन था। नगर के सारे दीपक बुझ गए थे, घर द्वारा बंद हो चुके थे। दो-एक सियारों को छोड़कर, अब इक्का-दुक्का लोगों या दूसरे प्राणियों का पता नहीं। उदयादित्य के शयन-कक्ष का द्वार बंद था। सहसा बाहर से कोई द्वार खटखटाने लगा।
घबराकर युवराज ने द्वार खोल दिए-‘‘क्या बात है बहन विभा ? क्या हुआ है ? इतनी रात गए यहां कैसे ?’’
विभा ने कहा-‘‘अब तक शायद सर्वनाश हो गया होगा।’’
सुरमा और उदयादित्य ने एक साथ पूछा-‘‘क्यों, क्या हुआ ?’’
विभा ने भय विकम्पित स्वर में धीरे से बताया। बताते-बताते वह अपने को संभाल न पाई और रो पड़ी-‘‘भैया अब क्या होगा ?’’
उदयादित्य ने कहा-‘‘मैं अभी जाता हूं।’’
विभा बोल उठी-‘‘नहीं-नहीं, मत जाओ।’’
उदयादित्य ने कहा-‘‘क्यों, विभा ?’’
‘‘पिताजी को अगर मालूम हो गया तो वे तुम पर और बिगड़ जाएंगे ?’’
सुरमा ने कहा-‘‘छिः विभा ! यह समय क्या यह सब सोचने का है ?’’
उदयादित्य ने वस्त्रादि पहने। कमर से तलवार बांधी और बाहर जाने की तैयारी करने लगे। विभा ने उनका हाथ पकड़कर कहा-‘‘भैया, तुम मत जाओ, किसी को भेज दो, मुझे बड़ा डर लग रहा है।’’
उदयादित्य ने कहा-‘‘विभा, इस समय रोको मत। अब समय नहीं है।’’
कहकर वे उसी क्षण बाहर निकल गए।
विभा सुरमा का हाथ पकड़कर बोल उठी-‘‘अब क्या होगा, भाभी ! पिताजी को यदि मालूम हो गया ? उन्होंने यदि भैया को दंड दिया ?’’
सुरमा ने कहा-‘‘और अब क्या हो जाएगा ? अब तो उनके स्नेह में कोई और कसर बाकी नहीं रही। जो कुछ रहा-सहा है, वह भी चला जाए, तो इसमें क्या बुराई है ?’’
विभा कांप उठी-‘‘मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है भाभी ! पिताजी ने....’’
सुरमा ने एक गहरी सांस भरकर कहा-‘‘मेरा तो विश्वास है कि संसार में जिसका कोई सहायक नहीं होता, नारायण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। हे प्रभु, ऐसा करना जिससे तुम्हारे नाम पर कलंक न लगे, मेरे इस विश्वास को तोड़ना मत प्रभु !’’
सुरमा ने कहा-‘‘प्रियतम, सब सहते रहो, धीरज रखो कभी-न-कभी तो सुख के दिन आएँगे ही।’’‘‘ मैं और कोई सुख नहीं चाहता।’’ उदयादित्य ने कहा-‘‘मैं तो यही चाहता हूं कि मैं राजप्रसाद में न जन्मा होता, युवराज न होता, यशोहर-अधिपति की क्षुद्रतम, तुच्छतम प्रजा की भी प्रजा होता, उनका ज्येष्ठ पुत्र-उनके सिंहासन, उनके समस्त धन, मान और यश-गौरव का एकमात्र उत्तराधिकारी न होता। कौन-सी तपस्या करूं जिससे यह समस्त अतीत उलटा जा सके।’’
सुरमा ने अत्यंत कातर होकर युवराज का दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उनके चेहरे की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। युवराज की मनोभिलाषा पूरी करने के लिए वह अपने प्राण भी दे सकती है, लेकिन दुख तो यही है कि प्राण देकर भी युवराज की इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता।
युवराज ने फिर कहा-‘‘सुरमा, राजा के घर जन्म लेने के कारण ही मैं सुखी न हो पाया। राजा के घर शायद उत्तराधिकारी ही जन्म लेते हैं, संतान के रूप में कोई जन्म नहीं लेता। पिता बचपन से ही प्रतिक्षण मेरी परीक्षा लेते आ रहे हैं कि मैं उनके द्वारा उपार्जित यशमान की रक्षा कर सकूंगा या नहीं, वंश का मुख उज्ज्वल कर सकूंगा या नहीं राज्य के भारी उत्तरदायित्व को संभाल सकूंगा या नहीं। उन्होंने मेरे प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक चेष्टा को परीक्षा की दृष्टि से देखा है, स्नेह की दृष्टि से नहीं। आत्मीयजन, मंत्री, राजसभासद और प्रजागण सभी मेरे प्रत्येक कार्य और मेरी प्रत्येक बात को कसौटी पर कस-कसकर मेरे भविष्य का आकलन करते रहे हैं। सबके सब सिर हिलाकर कहते हैं-उहूं, इस संकट में मैं राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं समझ पाता। सब मेरी अवहेलना करने लगे। पिताजी मुझसे घृणा करने लगे। यहां तक कि मुझसे उन्हें कोई आशा ही नहीं रह गई। मेरी खोज-खबर तक नहीं लेते।’’
सुरमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा-‘‘हाय, उनसे रहा कैसे जाता है ?’’
उसे दुख हुआ, उसे गुस्सा आया, ‘जो तुम्हें अबोध समझते हैं, वे स्वयं ही अबोध हैं।’
उदयादित्य धीरे से मुस्कराए। सुरमा की ठोड़ी पकड़कर उन्होंने गुस्से से लाल हो आए उसके मुखड़े को थपथपा दिया। दूसरे ही क्षण गम्भीर होकर बोले-‘‘नहीं सुरमा, राजकाज चलाने की बुद्धि सचमुच मुझमें नहीं। यह सिद्ध हो चुका है। जब मैं सोलह वर्ष का था, शासन-प्रबंध की शिक्षा देने के लिए महाराज ने हुसेनखाली परगने का भार मुझे सौंपा था। छः महीने में ही बड़ी गड़बड़ी शुरू हो गई। राजस्व घटने लगा, लेकिन प्रजा आशीर्वाद देने लगी। राज-कर्मचारी मेरे विरुद्ध महाराज से शिकायतें करने लगे। राजसभा के सभी सदस्यों की एक ही राय स्थापित हो गई कि युवराज चूंकि प्रजा के इतने प्रिय-पात्र हो गए हैं, इसलिए अब वे राज का शासन किसी भी प्रकार नहीं कर सकते। उस दिन से महाराज मेरी ओर देखते तक नहीं। वे कहते रहे, यह कुलांगार रायगढ़ के बूढ़े बसंतराय के समान ही होगा, सितार बजाकर नाचता फिरेगा और सारे राज्य को चौपट करके रख देगा।’’
सुरमा ने फिर कहा-‘‘प्रियतम, थोड़ा धीरज रखो। आखिर वे आपके पिता हैं। इस समय राज्य-उपार्जन और राज्य वृद्धि की एकमात्र दुराशा से उनका हृदय विचलित है, वहां स्नेह के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। जितनी दूर तक उनकी अभिलाषा पूरी होती रहेगी, उनके स्नेह के साम्राज्य में भी उतनी ही बढ़ोत्तरी होती रहेगी।’’
युवराज ने कहा-‘‘तुम्हारी बुद्धि तीव्र और दूरदर्शी है, सुरमा, किंतु इस बार तुम गलत समझ रही हो। एक तो अभिलाषा का कोई अंत नहीं, दूसरे पिताजी के राज्य की सीमा जितनी ही बढ़ती जाएगी उसके हाथ से निकल जाने का उनका भय भी उतना ही बढ़ता जाएगा और मुझे वे उतना ही अधिक उसके अनुपयुक्त समझते जाएंगे।’’
सुरमा ने गलत नहीं समझा था, केवल गलत विश्वास किया करती थी और विश्वास बुद्धि को भी लांघ जाता है। वह संपूर्ण मन से चाहती रही कि ऐसा ही हो।
उदयादित्य बिना रुके कहते गए-‘‘चारों ओर कहीं कृपादृष्टि और कहीं अवहेलना सहन न कर पाता तो मैं बीच-बीच में भागकर राजगढ़ दादा साहब के पास चला जाता था। पिताजी तो कभी खोज-खबर लेते नहीं थे। ओह, वहां जाते ही कैसा परिवर्तन हो जाता था। वहां पेड़-पौधे और बाग-बगीचे देखने को मिलते, ग्रामीणों के झोंपड़ों में जा सकता था। दिन-रात राजवेश धारण किए नहीं रहना पड़ता था। इसके अलावा जहां दादा साहब रहते हैं, वहां विषाद, चिंता और कठोर गांभीर्य फटने भी नहीं पाता था। वे गा-बजाकर, आमोद-प्रमोद कर चारों दिशाओं को गुंजायमान किए रहते थे। उनके चारों ओर प्रसन्नता, शांति और सद्भावना विराजती थी। वहां जाकर मैं भूल जाता कि मैं यशोहर का युवराज हूं। कितनी सुखद भूल होती थी वह ! और एक दिन जब मेरी उम्र अट्ठारह वर्ष की रही होगी, रायगढ़ में तब बसंती हवा चल रही थी, तभी एक सघन निकुंज में मैंने रुक्मिणी को देखा...।’’
सुरमा बोल उठी-‘‘यह बात तो मैं कई बार सुन चुकी हूं।’’
उदयादित्य ने कहा-‘‘और एक बार सुन लो। रह-रहकर उस समय की एक-एक बात हृदय को कचोटती रहती है। यदि कहकर इसे बाहर न निकाल दूं तो भी प्राण बचेंगे कैसे ! और यह बात तुम्हें बताते हुए अब भी संकोच और कष्ट का अनुभव होता है, इसी से बार-बार कहा करता हूं, जिस दिन कहने में संकोच और कष्ट न होगा, उस दिन समझ लूंगा कि मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ, और तब उसकी चर्चा कभी नहीं करूंगा।’’
सुरमा ने कहा-‘‘प्रायश्चित किस बात का, प्रियतम ? यदि तुमने पाप भी किया हो तो वह पाप का दोष है, तुम्हारा दोष नहीं। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती ? क्या अन्तर्यामी तुम्हारे मन को देख नहीं पाते ?’’
उदयादित्य ने सुरमा की बात अनसुनी करके कहा-‘‘रुक्मिणी मुझसे उम्र में तीन वर्ष बड़ी थी। बेचारी, अकेली और विधवा। दादा साहब के अनुग्रह के कारण वह किसी तरह रायगढ़ में टिक पाई थी। नहीं जानता कि किस कौशल से उसने मुझे अपनी ओर पहली बार में ही आकर्षित कर लिया था। उस समय मेरे मन में दोपहर की धूप खिल रही थी। इतना प्रखर आलोक था कि मैं कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। चारों ओर सृष्टि ज्योतिर्मय भाप से आच्छादित प्रतीत होती थी। शरीर का समस्त रक्त मानो सिर पर चढ़ गया था, कुछ भी विचित्र और असंभव नहीं लगता था, पथ-कुपथ, दिशा-अदिशा सब कुछ एकाकार प्रतीत होते थे। उससे पूर्व कभी मेरी ऐसी दशा नहीं हुई, उसके बाद भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। जगदीश्वर ही जानें, उन्होंने अपने किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस क्षुद्र, दुर्बल हृदय के विरुद्ध, एक दिन के लिए समस्त जगत को इस प्रकार उत्तेजित कर दिया कि सचराचर सृष्टि एकतंत्र होकर इस हृदय को क्षण में विपथ की ओर बहा ले गई। अधिक नहीं, केवल क्षण भर के लिए समस्त बहिर्जगत का एक क्षण स्थायी और दारुण आघात लगा और उसी क्षण में यह दुर्बल हृदय जड़ से उखड़ गया-विद्युत-वेग से वह धूल में जा गिरा। उसके बाद जब वह उठा तो धूल-धूसरित और म्लान था-वह धूल फिर पुछ नहीं सकी, उस मलिनता का चिन्ह फिर नहीं मिटा। मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया था कि विधाता ने एक क्षण में मेरे जीवन की समस्त उज्ज्वलता को काला कर दिया ? दिन को रात में परिवर्तित कर दिया। मेरे हृदय के पुष्पोद्यान में खिल रहे मालती और जूही के विहंसते मुखड़े भी ग्लानि से मलिन पड़ गए।’’
कहते-कहते उदयादित्य का गोरा चेहरा आरक्त हो उठा, आंखें फैल गईं, सिर से लेकर पांवों तक बिजली-सी कौंध गई जैसे।
सुरमा ने हर्ष, गर्व और कष्ट से सिहरकर कहा-‘‘ अब इसे रहने भी दो, तुम्हें मेरे सिर की सौगंध !’’
लेकिन उदयादित्य कहते ही गए-‘‘धीरे-धीरे रक्त की उष्णता शांत हुई और तब मैं सारी वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखने लगा। जब विश्व विक्षुब्ध और बौखलाए, डोलते-डगमगाते और सुर्ख आंखों वाले किसी पागल के दिमाग में चक्करघिन्नी खाती हवाई सनक की तरह नहीं बल्कि स्वाभाविक कार्यक्षेत्र के रूप में दिखाई देने लगा तो मन की न जाने कैसी अवस्था हो गई थी। तब पहली बार पता चला कि कहां आ गिरा हूं। हजारों-लाखों कोस नीचे पाताल के गहन गह्वर में, अंधतम रजनी के बीच पलक झपकते ही आ गिरा हूं। तब दादा साहब स्नेहपूर्वक बुला ले गए। भला मैं उनको अपना मुंह दिखा ही कैसे पाया। लेकिन उसी समय मुझे रायगढ़ छोड़ देना पड़ा। दादा साहब मुझे देखे बिना रह नहीं सकते थे। वे मुझे बराबर बुलावा भेजते। परंतु मेरे मन में ऐसा डर समा गया था कि जाते नहीं बना। तब वे स्वयं मुझे बहन विभा को देखने के लिए आने लगे। कोई अभिमान नहीं, कोई उलाहना नहीं। इतना भी नहीं पूछते कि मैं क्यों नहीं जाता। हमसे मिलते, हंसी-खुशी मनाते और लौट जाते।’’
उदयादित्य ने किंचित् मुस्कराकर अतिशय मृदुल कोमल प्रेम से अपने बड़े-बड़े तरल नेत्रों से सुरमा की ओर देखा। सुरमा समझ गई कि इस बार कौन-सी बात छिड़ने वाली है। उसका चेहरा झुक गया, वह कुछ चंचल हो उठी। युवराज ने दोनों हाथों से सुरमा के कपोलों को पकड़कर चेहरे को ऊपर उठाया फिर उससे सटकर बैठ गए और धीरे से उसके मुख-मंडल को अपने कंधे पर रख लिया। बाएं हाथ से उसकी कमर को पकड़ते हुए, गंभीर, प्रशांत, प्रेम से गाल को चूमकर उन्होंने कहा-‘‘उसके बाद क्या हुआ, बताओ तो सुरमा ? तुम्हारा यह बुद्धि से दीप्त, स्नेह-प्रेम से कोमल, हास्योज्ज्वल, प्रशांतभाव से विमल मुखड़ा, कहां से उदित हुआ ? मेरे मन में उस घनान्धकार के दूर होने की क्या कोई आशा थी ? तुम मेरी ऊषा हो, मेरा प्रकाश, मेरी आशा ! किस माया-मंत्र से तुमने उस अंधकार को मिटा दिया ?’’
युवराज बार-बार सुरमा का मुंह चूमने लगे। वह कुछ न बोली, आनंदातिरेक से उसकी आंखें भर आईं।
युवराज ने कहा-‘‘इतने दिनों के बाद मुझे सच्चा आश्रय मिला। तुम्हीं से प्रथम बार सुना कि मैं अबोध नहीं। उस पर विश्वास किया और स्वयं को वैसा ही समझने लगा। तुम्हीं से यह सीखा कि बुद्धि किसी अंधेरी संकरी गली के समान टेढ़ी-मेढ़ी और ऊंची-नीची नहीं, राजपथ की तरह सीधी, समतल और प्रशस्त होती है। पहले मैं अपने-आपसे घृणा करता था, स्वयं अपनी अवहेलना किया करता था। कोई काम करने का साहस नहीं कर पाता था। मन यदि कहता कि वह ठीक है तो आत्मसंशयी संस्कार कह उठता था कि शायद वह ठीक हो। जो जैसा व्यवहार करता था, सह लिया करता था। इतने दिनों के बाद समझ पाया कि मैं भी कुछ हूं। इतने दिनों तक मैं अदृश्य था जैसे तुमने मुझे बाहर निकाला। सुरमा, तुमने मेरा अविष्कार किया है। अब मेरा मन जिसे अच्छा कहता है, उचित समझता है, मैं उसे उसी क्षण करना चाहता हूं। तुम्हारे ऊपर मेरा इतना विश्वास है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मैं भी अपने-आप पर निर्भय होकर विश्वास कर पाता हूं। इस सुकोमल शरीर में इतनी शक्ति कहां छिपी थी, जिससे तुमने मुझे भी इतना शक्तिसंपन्न बना दिया ?’’
पूर्ण समर्पण के भाव से सुरमा पति के वक्षस्थल से लिपट गई। असीम उत्सर्गमयी दृष्टि से वह पति की ओर निहारती रही, मानो उसके नेत्र कह रहे हों, ‘मेरा और कोई नहीं, केवल तुम्हीं से मेरा सर्वस्व है।’
बचपन से उदयादित्य आत्मीयजनों की उपेक्षा सहते आए हैं, इसीलिए बीच-बीच में कभी-कभी निस्तब्ध गहन रात्रि में, सुरमा के समीप बैठकर सौ बार कही हुई उसी पुरानी जीवन-कथा को खंड-खंड कर कहना और फिर एक-एक बात की आलोचना करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है।
उदयादित्य ने कहा-‘‘इस तरह और कितने दिन चलेगा, सुरमा ! इधर राज्यसभा के सभासदगण एक प्रकार की दयाभरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हैं। उधर अंतःपुर में मां तुम्हें अपमानित करती रहती हैं। यहां तक कि दास-दासी भी तुम्हारा सम्मान नहीं करते। मैं किसी को अपनी बात बता नहीं पाता और चुपचाप सहता रहता हूं। तेजस्विनी होकर भी तुम चुपचाप सब कुछ सह लिया करती हो। मेरे कारण तुम्हें केवल अपमान और कष्ट ही सहना पड़ रहा है, इससे तो यही अच्छा था कि हमारा विवाह ही न होता।’’
सुरमा बोली-‘‘यह क्यों कहते हो, स्वामी ! ऐसे ही समय में तो तुम्हें सुरमा की आवश्यकता है। सुख के समय तो सुरमा विलास की वस्तु और क्रीड़ा की कठपुतली होती। समस्त दुखों का अतिक्रमण कर मेरे मन में यही सुख जाग रहा है कि मैं तुम्हारे काम आ रही हूं, तुम्हारे साथ दुख सहने में जो अतुल आनंद प्राप्त होता है, मैं उसी का उपभोग कर रही हूं। दुख केवल इस बात का है कि तुम्हारे समस्त कष्टों को मैं क्यों नहीं झेल पाती ?’’
युवराज कुछ देर चुप रहे, फिर बोले-‘‘दुख ? मुझे अपने लिए तो उतनी चिंता नहीं। अब सब कुछ सह्य हो गया है। दुख यही है कि मेरे लिए तुम्हें अपमान सहना पड़ता है, क्यों भला ? एक सच्ची नारी की भांति दुख में तुमने मुझे सांत्वना दी है, थक जाने पर विश्राम दिया है, लेकिन मैं एक पति की तरह तुम्हें अपमानित और लज्जित होने से नहीं बचा सका। तुम्हारे पिता श्रीपुरराज मेरे पिता को अपना अधिपति नहीं मानते, वे यशोहर की अधीनता स्वीकार नहीं करते, इसलिए मेरे पिता तुम्हारा निरादर कर अपने बड़प्पन को बनाए रखना चाहते हैं। अगर कोई तुम्हारा अपमान भी करे तो उस पर ध्यान नहीं देते। वे समझते हैं कि तुम्हें पुत्रवधू बनाया, यही बहुत ज्यादा हुआ, अब अधिक सहा नहीं जाता। कभी-कभी मन में आता है कि सब कुछ छोड़-छाड़कर तुम्हें लेकर कहीं अन्यत्र चला जाऊं। अब तक संभवतः चला भी जाता, केवल तुमने पकड़ रखा है।’’
रात बहुत बीत गई थी। संध्याकाल में उगने वाले कई तारे अस्त हो चुके थे। और गहन रात्रि में उगने वाले तारे चमक उठे थे। प्राकार-तोरण पर स्थित प्रहरियों की पदचाप दूर से ही सुनाई दे रही थी। सारा संसार गहरी निद्रा में लीन था। नगर के सारे दीपक बुझ गए थे, घर द्वारा बंद हो चुके थे। दो-एक सियारों को छोड़कर, अब इक्का-दुक्का लोगों या दूसरे प्राणियों का पता नहीं। उदयादित्य के शयन-कक्ष का द्वार बंद था। सहसा बाहर से कोई द्वार खटखटाने लगा।
घबराकर युवराज ने द्वार खोल दिए-‘‘क्या बात है बहन विभा ? क्या हुआ है ? इतनी रात गए यहां कैसे ?’’
विभा ने कहा-‘‘अब तक शायद सर्वनाश हो गया होगा।’’
सुरमा और उदयादित्य ने एक साथ पूछा-‘‘क्यों, क्या हुआ ?’’
विभा ने भय विकम्पित स्वर में धीरे से बताया। बताते-बताते वह अपने को संभाल न पाई और रो पड़ी-‘‘भैया अब क्या होगा ?’’
उदयादित्य ने कहा-‘‘मैं अभी जाता हूं।’’
विभा बोल उठी-‘‘नहीं-नहीं, मत जाओ।’’
उदयादित्य ने कहा-‘‘क्यों, विभा ?’’
‘‘पिताजी को अगर मालूम हो गया तो वे तुम पर और बिगड़ जाएंगे ?’’
सुरमा ने कहा-‘‘छिः विभा ! यह समय क्या यह सब सोचने का है ?’’
उदयादित्य ने वस्त्रादि पहने। कमर से तलवार बांधी और बाहर जाने की तैयारी करने लगे। विभा ने उनका हाथ पकड़कर कहा-‘‘भैया, तुम मत जाओ, किसी को भेज दो, मुझे बड़ा डर लग रहा है।’’
उदयादित्य ने कहा-‘‘विभा, इस समय रोको मत। अब समय नहीं है।’’
कहकर वे उसी क्षण बाहर निकल गए।
विभा सुरमा का हाथ पकड़कर बोल उठी-‘‘अब क्या होगा, भाभी ! पिताजी को यदि मालूम हो गया ? उन्होंने यदि भैया को दंड दिया ?’’
सुरमा ने कहा-‘‘और अब क्या हो जाएगा ? अब तो उनके स्नेह में कोई और कसर बाकी नहीं रही। जो कुछ रहा-सहा है, वह भी चला जाए, तो इसमें क्या बुराई है ?’’
विभा कांप उठी-‘‘मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है भाभी ! पिताजी ने....’’
सुरमा ने एक गहरी सांस भरकर कहा-‘‘मेरा तो विश्वास है कि संसार में जिसका कोई सहायक नहीं होता, नारायण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। हे प्रभु, ऐसा करना जिससे तुम्हारे नाम पर कलंक न लगे, मेरे इस विश्वास को तोड़ना मत प्रभु !’’
2
‘‘महाराज, यह कहा क्या ठीक होगा
?’’ मंत्री ने कहा।
प्रतापदित्य ने पूछा-‘‘कौन-सा काम ?’’
मंत्री ने उत्तर दिया-‘‘कल आपने जो आदेश दिया था।’’
प्रतापादित्य ने खिन्न होकर पूछा-‘‘कल क्या आदेश दिया था ?’’
मंत्री ने कहा-‘‘अपने चाचा के संबंध में।’’
प्रतापादित्य ने और भी विरक्त स्वर में कहा-‘‘चाचा के बारे में क्या ?’’
मंत्री बोले-‘‘महाराज ने आदेश दिया था कि बसंतराय जब यशोहर आते हुए रात्रि में शिमुलतली वाली सराय में ठहरें हों, तब..’’
प्रतापादित्य ने भौंहें सिकोड़कर कहा-‘‘तब क्या ? हमेशा पूरी बात कहा करो।’’
‘‘तब दो पठान जाकर...’’
प्रतापादित्य-‘‘हां, फिर ?’’
‘‘उन्हें मार डालें।’’
प्रतापादित्य ने नाराज होकर कहा-‘‘मंत्री, क्या तुम अचानक बच्चे हो गए हो ? एक बात पूछने के लिए दस सवाल करने पड़ते हैं भला । असल बात मुंह पर लाते संकोच हो नहीं रहा है ? राज-काज में मन लगने की तुम्हारी उमर बीत गई और शायद परलोक की चिंता करने के दिन आ गए। आश्चर्य है, अब तक तुमने कार्य-भार से मुक्त होने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं की।’’
मंत्री ने कहा-‘‘महाराज मेरी बात को अच्छी तरह समझ नहीं सके हैं शायद !
प्रतापादित्य बोले-‘‘मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, जिस काम को मैं कर सकता हूं, उसे तुम जबान पर भी नहीं ला सकते, क्यों ? तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूं, उसे करने का कोई-न-कोई गंभीर कारण अवश्य होगा। मैंने उसके संबंध में धर्म-अधर्म उचित-अनुचित सब कुछ अच्छी तरह सोच लिया है।’’
मंत्री ने सहमकर कहा-‘‘जी हां, महाराज ! मैं...’’
प्रतापादित्य घुड़ककर बोल-‘‘चुप रहो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो ! जब मैं इस काम को-अपने सगे चाचा की हत्या करने को-उद्यत हुआ हूं तो इस संबंध में निस्संदेह तुम्हारी अपेक्षा मैंने बहुत अधिक सोचा होगा। इस काम में कोई अधर्म नहीं है। इसे अच्छी तरह समझ लो, मेरा यही व्रत है कि जिन म्लेच्छों ने हमारे देश में आकर अनाचार आरंभ किया है, जिनके अत्याचारों से हमारे देश से सनातम आर्यधर्म लुप्त होता जा रहा है, क्षत्रिय मुगलों को अपनी कन्याएं देने लगे हैं, हिंदू आचारभ्रष्ट हो रहे हैं, उन म्लेच्छों को मैं यहां से निकाल बाहर करूंगा और अपने आर्यधर्म को राहु-ग्रास से मुक्त करूंगा। इस व्रत की पूर्ति के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि इस काम के लिए समस्त बंगदेश के राजा मेरी अधीनता में एक हो जाएं। जो यवनों के मित्र हैं, उनका विनाश किए बिना इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। चाचा बसंतराय मेरे पूजनीय हैं, लेकिन सच कहने में कोई पाप नहीं, वे हमारे वंश के कलंक हैं। उन्होंने स्वयं को म्लेच्छों का दास मान लिया है। ऐसे लोगों से प्रतापादित्य का कोई रिश्ता नहीं। सड़ जाने पर अपनी ही भुजा को काटकर फेंक देना पड़ता है। मेरी इच्छा है कि रायवंश की सड़ांध, बंगदेश की सड़ांध, उस बसंतराय को काटकर फेंक दिया जाए, और ऐसा करके रायवंश तथा बंगदेश की रक्षा की जाए।’’
प्रतापदित्य ने पूछा-‘‘कौन-सा काम ?’’
मंत्री ने उत्तर दिया-‘‘कल आपने जो आदेश दिया था।’’
प्रतापादित्य ने खिन्न होकर पूछा-‘‘कल क्या आदेश दिया था ?’’
मंत्री ने कहा-‘‘अपने चाचा के संबंध में।’’
प्रतापादित्य ने और भी विरक्त स्वर में कहा-‘‘चाचा के बारे में क्या ?’’
मंत्री बोले-‘‘महाराज ने आदेश दिया था कि बसंतराय जब यशोहर आते हुए रात्रि में शिमुलतली वाली सराय में ठहरें हों, तब..’’
प्रतापादित्य ने भौंहें सिकोड़कर कहा-‘‘तब क्या ? हमेशा पूरी बात कहा करो।’’
‘‘तब दो पठान जाकर...’’
प्रतापादित्य-‘‘हां, फिर ?’’
‘‘उन्हें मार डालें।’’
प्रतापादित्य ने नाराज होकर कहा-‘‘मंत्री, क्या तुम अचानक बच्चे हो गए हो ? एक बात पूछने के लिए दस सवाल करने पड़ते हैं भला । असल बात मुंह पर लाते संकोच हो नहीं रहा है ? राज-काज में मन लगने की तुम्हारी उमर बीत गई और शायद परलोक की चिंता करने के दिन आ गए। आश्चर्य है, अब तक तुमने कार्य-भार से मुक्त होने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं की।’’
मंत्री ने कहा-‘‘महाराज मेरी बात को अच्छी तरह समझ नहीं सके हैं शायद !
प्रतापादित्य बोले-‘‘मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, जिस काम को मैं कर सकता हूं, उसे तुम जबान पर भी नहीं ला सकते, क्यों ? तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूं, उसे करने का कोई-न-कोई गंभीर कारण अवश्य होगा। मैंने उसके संबंध में धर्म-अधर्म उचित-अनुचित सब कुछ अच्छी तरह सोच लिया है।’’
मंत्री ने सहमकर कहा-‘‘जी हां, महाराज ! मैं...’’
प्रतापादित्य घुड़ककर बोल-‘‘चुप रहो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो ! जब मैं इस काम को-अपने सगे चाचा की हत्या करने को-उद्यत हुआ हूं तो इस संबंध में निस्संदेह तुम्हारी अपेक्षा मैंने बहुत अधिक सोचा होगा। इस काम में कोई अधर्म नहीं है। इसे अच्छी तरह समझ लो, मेरा यही व्रत है कि जिन म्लेच्छों ने हमारे देश में आकर अनाचार आरंभ किया है, जिनके अत्याचारों से हमारे देश से सनातम आर्यधर्म लुप्त होता जा रहा है, क्षत्रिय मुगलों को अपनी कन्याएं देने लगे हैं, हिंदू आचारभ्रष्ट हो रहे हैं, उन म्लेच्छों को मैं यहां से निकाल बाहर करूंगा और अपने आर्यधर्म को राहु-ग्रास से मुक्त करूंगा। इस व्रत की पूर्ति के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि इस काम के लिए समस्त बंगदेश के राजा मेरी अधीनता में एक हो जाएं। जो यवनों के मित्र हैं, उनका विनाश किए बिना इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। चाचा बसंतराय मेरे पूजनीय हैं, लेकिन सच कहने में कोई पाप नहीं, वे हमारे वंश के कलंक हैं। उन्होंने स्वयं को म्लेच्छों का दास मान लिया है। ऐसे लोगों से प्रतापादित्य का कोई रिश्ता नहीं। सड़ जाने पर अपनी ही भुजा को काटकर फेंक देना पड़ता है। मेरी इच्छा है कि रायवंश की सड़ांध, बंगदेश की सड़ांध, उस बसंतराय को काटकर फेंक दिया जाए, और ऐसा करके रायवंश तथा बंगदेश की रक्षा की जाए।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i