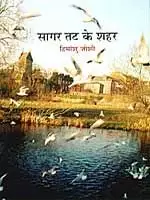|
कहानी संग्रह >> सागर तट के शहर सागर तट के शहरहिमांशु जोशी
|
301 पाठक हैं |
|||||||
आधुनिक कहानियों का संग्रह।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
हिमांशु जोशी का कथा-संसार स्वयं में बहुत व्यापक और विस्तृत है। अनेक
आयामों को छूती हैं उनकी रचनाएं। उनमें सरलता, सहजता ही नहीं, जीवन का वह
यथार्थ भी है, जो किसी कृति को सार्थक बनाता है, एक नयी पहचान देकर।
अनुभव और अनुभूतियों का जीवन्त रेखाओं से उकेरे ये चौदह चित्र अनेक प्रश्न ही नहीं जगाते बल्कि समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। इनके सजीव पात्रों के आईने में जो संसार प्रतिबिम्बित होता है, वह कहीं अपना-सा लगने लगता है- जैसे अपनी ही अनुभूतियों के अनेक अक्स।
कहानी मात्र कहानी न रहकर यथार्थ भी बन जाए, यह स्वयं में एक उपलब्धि है। आज की वास्तविकताएं इन रचनाओं में नाना रूपों एवं रंगों में उजागर होकर बहुत कुछ सोचने के लिए विविश करती हैं।
वर्तमान कहानियों के बीच अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाती ये सहज रचनाएँ, जिस रूप में स्वयं को परिभाषित करती हैं, वह चौंकाता ही नहीं, गम्भीर विमर्श की जमीन भी तैयार करता है। आने वाले कल की कहानी का स्वरूप भी इनमें झलकता हुआ मिलता है, जहाँ विधाएँ बन्धनमुक्त होकर एक नयी विधा की सृष्टि करती हैं।
अनुभव और अनुभूतियों का जीवन्त रेखाओं से उकेरे ये चौदह चित्र अनेक प्रश्न ही नहीं जगाते बल्कि समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। इनके सजीव पात्रों के आईने में जो संसार प्रतिबिम्बित होता है, वह कहीं अपना-सा लगने लगता है- जैसे अपनी ही अनुभूतियों के अनेक अक्स।
कहानी मात्र कहानी न रहकर यथार्थ भी बन जाए, यह स्वयं में एक उपलब्धि है। आज की वास्तविकताएं इन रचनाओं में नाना रूपों एवं रंगों में उजागर होकर बहुत कुछ सोचने के लिए विविश करती हैं।
वर्तमान कहानियों के बीच अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाती ये सहज रचनाएँ, जिस रूप में स्वयं को परिभाषित करती हैं, वह चौंकाता ही नहीं, गम्भीर विमर्श की जमीन भी तैयार करता है। आने वाले कल की कहानी का स्वरूप भी इनमें झलकता हुआ मिलता है, जहाँ विधाएँ बन्धनमुक्त होकर एक नयी विधा की सृष्टि करती हैं।
अथ
कहानी का कहानी न होना ही कहानी होना है।
समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है और बदल रही है, हमारी सोच, हमारी जीवन-शैली, जीवन एवं जगत के प्रति हमारा दृष्टिकोण। लगता है वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया में सब सिमटकर, एक-दूसरे में विलीन हो रहे हैं।
साहित्य की विधाएँ भी नये-नये रूपों में परिभाषित हो रही हैं। कहानी, कहानी तक सीमित न रहकर, विशुद्ध सच का पर्याय भी बन रही हैं। जीवनियाँ जीवन्त-कथाओं का रूप ले रही हैं। आत्मकथाएं औपन्यासिक शैली में पाठकों को अधिक रिझा रही हैं। यानी जो जैसा है हमें उस रूप की अपेक्षा किसी दूसरे रूप में देखना अधिक स्वाभाविक लग रहा है। कहानी का सच भी जीवन के सच का ही दूसरा रूप बनकर उभर रहा है।
विधाओं की सीमा-रेखाओँ के टूटने से साहित्य एक नया आकार ले रहा है, जिसमें कम कृत्रिमता और अधिक आत्मीयता यानी अनुभूति की प्रामाणिकता अधिक सहज लग रही है।
प्रस्तुत संग्रह में गत कुछ वर्षों की अवधि में लिखी मेरी कुछ कहानियाँ हैं। जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ, वह इनके माध्यम से अभिव्यक्त हो सका तो लगेगा कि मेरा यह सहज प्रयास सफल रहा।
‘अगला यथार्थ’ का अगला यथार्थ, ‘एक बार फिर’ का सन्त्रास’ ‘अग्निपथ’ की दहकती पीड़ा, ‘एक सार्थक सच’ की विडम्बनाएँ अनेक प्रश्नों एवं प्रश्न-चिन्हों की ओर इंगित करती हैं। ह्वेनसाँग...’
का त्रासद सत्य आज के अभिशप्त इतिहास को जिस तरह परिभाषित करता है, वह दूर तक आहत किये बिना नहीं रहता। क्रूरता की यह काल कथा आखिर किस दिशा में ले जाने के लिये विवश कर रही है ?
‘दाह’ का दारुण हमें किस कगार की ओर ढकेल रहा है ? बस्ती की बस्तियाँ, गाँव के गाँव उजड़ रहे हैं ? क्यों ?
जो वट-वृक्ष कभी तपती धूप में, अपनी शीतल छाँह में प्राणियों को त्राण देते थे, वे स्वयं झुलसे हुए, साये की तलाश में दम तोड़ रहे हैं। ‘आश्रम’ का सच, छटपटाती आस्था, मरते ममत्व एवं विषमताओं के वैषम्य का मात्र मूक साक्षी बनकर रह जाता है ? क्यों ?
‘सागर तट के शहर’ में सागर तट के शहर कई-कई रूपों एवं रंगों में उभर कर समाने आते हैं। वे जिस सत्य से साक्षात्कार कराते हैं, वह सत्य भी क्या हमारा ही अपना आत्मीय सत्य नहीं ? मृगतृष्णा है। जल है। जल का एहसास है। पर निपट, निश्छल, निर्व्याज मानवीय सम्बन्धों से बड़ा भी क्या कोई और सम्बन्ध हो सकता है ?
सहज रूप में, सहज बात कहना शायद कहीं बहुत कठिन होता है। कहानी का सच जीवन के सच का भी पर्याय बन जाय इससे बड़ी उपलब्धि किसी रचना के लिये और क्या हो सकती है ?
समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है और बदल रही है, हमारी सोच, हमारी जीवन-शैली, जीवन एवं जगत के प्रति हमारा दृष्टिकोण। लगता है वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया में सब सिमटकर, एक-दूसरे में विलीन हो रहे हैं।
साहित्य की विधाएँ भी नये-नये रूपों में परिभाषित हो रही हैं। कहानी, कहानी तक सीमित न रहकर, विशुद्ध सच का पर्याय भी बन रही हैं। जीवनियाँ जीवन्त-कथाओं का रूप ले रही हैं। आत्मकथाएं औपन्यासिक शैली में पाठकों को अधिक रिझा रही हैं। यानी जो जैसा है हमें उस रूप की अपेक्षा किसी दूसरे रूप में देखना अधिक स्वाभाविक लग रहा है। कहानी का सच भी जीवन के सच का ही दूसरा रूप बनकर उभर रहा है।
विधाओं की सीमा-रेखाओँ के टूटने से साहित्य एक नया आकार ले रहा है, जिसमें कम कृत्रिमता और अधिक आत्मीयता यानी अनुभूति की प्रामाणिकता अधिक सहज लग रही है।
प्रस्तुत संग्रह में गत कुछ वर्षों की अवधि में लिखी मेरी कुछ कहानियाँ हैं। जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ, वह इनके माध्यम से अभिव्यक्त हो सका तो लगेगा कि मेरा यह सहज प्रयास सफल रहा।
‘अगला यथार्थ’ का अगला यथार्थ, ‘एक बार फिर’ का सन्त्रास’ ‘अग्निपथ’ की दहकती पीड़ा, ‘एक सार्थक सच’ की विडम्बनाएँ अनेक प्रश्नों एवं प्रश्न-चिन्हों की ओर इंगित करती हैं। ह्वेनसाँग...’
का त्रासद सत्य आज के अभिशप्त इतिहास को जिस तरह परिभाषित करता है, वह दूर तक आहत किये बिना नहीं रहता। क्रूरता की यह काल कथा आखिर किस दिशा में ले जाने के लिये विवश कर रही है ?
‘दाह’ का दारुण हमें किस कगार की ओर ढकेल रहा है ? बस्ती की बस्तियाँ, गाँव के गाँव उजड़ रहे हैं ? क्यों ?
जो वट-वृक्ष कभी तपती धूप में, अपनी शीतल छाँह में प्राणियों को त्राण देते थे, वे स्वयं झुलसे हुए, साये की तलाश में दम तोड़ रहे हैं। ‘आश्रम’ का सच, छटपटाती आस्था, मरते ममत्व एवं विषमताओं के वैषम्य का मात्र मूक साक्षी बनकर रह जाता है ? क्यों ?
‘सागर तट के शहर’ में सागर तट के शहर कई-कई रूपों एवं रंगों में उभर कर समाने आते हैं। वे जिस सत्य से साक्षात्कार कराते हैं, वह सत्य भी क्या हमारा ही अपना आत्मीय सत्य नहीं ? मृगतृष्णा है। जल है। जल का एहसास है। पर निपट, निश्छल, निर्व्याज मानवीय सम्बन्धों से बड़ा भी क्या कोई और सम्बन्ध हो सकता है ?
सहज रूप में, सहज बात कहना शायद कहीं बहुत कठिन होता है। कहानी का सच जीवन के सच का भी पर्याय बन जाय इससे बड़ी उपलब्धि किसी रचना के लिये और क्या हो सकती है ?
हिमांशु जोशी
अगला यथार्थ
कितना कुछ नहीं था मन में, यहाँ आते समय ? कितने भाव, कितने विचार ! जो
सन्तोष के साथ –साथ कहीं गहरे सन्ताप के भी कारण थे- जिन्दगी-भर
नासूर की तरह रिसते हुए....
पर यहां आकर वह एक तरह से गूँगा-सा क्यों हो गया है ?
अचरज भरी निगाहों से वह चारों ओर देखता है- हर रोज उमड़ते-घुमड़ते काले बादलों को। चारों दिशाओं में बिखरे जल, जल-ही-जल को। अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो, जब बादल न घिरे हों, न गरजे हों, न बरसे हों। थोड़ी-सी झड़ी के बाद फिर एकाएक साफ आसमान। धुली धरती। ठीक सिर पर टकराती चुभती हुई उजली धूप !
अथाह पानी में तैरती-सी हरियाली की हरी-हरी क्यारियाँ ! दूर-दूर तक छिटके छोटे-छोटे द्वीप ! सामने वाला राँस द्वीप तो ऐसा लगता, जैसे हाथ बढ़ाकर छू लेगा ....
वह घण्टों विस्फारित नेत्रों से उन्हें निहारता, न जाने क्या-क्या सोचता रहता है ! परछाइयों की तरह कई आकृतियाँ उभरती-मिटती हैं। स्याह-सफेद कई-कई चित्र !
निर्जन -से इन द्वीपों में से उसे अजनबीपन के साथ-साथ कहीं अपनेपन का कोई अदृश्य रिश्ता-सा भी लगता है।
धरती के कण-कण से एक अव्यक्त गहरा आत्मभाव !
एक लम्बी निःश्वास के साथ, वह आँखें मूँद लेता है।
सच, तब कितना भयानक होगा, वहाँ का वातावरण ! कल रात देर तक वह उस जेट्टी के पास खड़ा रहा। जहाँ कलकत्ता से आनेवाले जलपोत रुका करते थे। कभी ऐसे ही एक जहाज से... एक दिन....ऐसे ही.....इसी तरह....
जब तक दादी जिन्दा थीं, बहकी-बहकी-सी कितनी बातें बतलाया करती थीं, जैसे आँखों देखा हाल सुना रही हों। ‘‘कालापानी में आकाश को छूते भयानक जंगल होते हैं रे ! जंगल–ही-जंगल ! साँपों, बिच्छुओं, जहरीले कीड़े-मकोड़ों से भरे ! जिनके काटे का आदमी पानी तक नहीं माँगता......वनों में खूँख्वार वन-मानुष, तीर-भाले चलाते हैं। आदमियों को भूनकर खा जाते हैं..... बिछौने पर, छतों की शहतीरों पर रस्सी की तरह साँप सरकते रहते हैं। धूल के कणों की तरह बारीक सफेद चींटियाँ देखते-देखते हाथी भी हजम कर जाती हैं।’’
अनपढ़ दादी को, जो जिन्दगी भर अपने गाँव से बाहर नहीं गयी, ये रोमांचक रहस्यपूर्ण बातें कहाँ से मालूम पड़ीं, पता नहीं। कहते हैं, पास के गाँव का एक लड़का अभी भागकर कलकत्ता गया था। वहाँ पुलिस में भर्ती हो गया था। कैदियों को लाने-ले-जाने के काम से दो-तीन बार कालापानी तक हो आया था। हो सकता है लौटकर उसी ने सुनायी हों ये बातें !
दादी कभी-कभी स्वयं से बड़बड़ातीं, ‘‘नाश हो इनका ! कहते हैं ये राकस गोरे, कैदियों की नंगी पीठ पर चाबुक मारते हैं। खाल उधेड़ देते हैं। शरीर लहूलुहान हो जाता है।... दिन–रात बरखा-घाम में भी काम ही काम, पर खाने को दो रूखी रोटियाँ तक नहीं.... तेरे दादाजी से तो भूख कतई बरदाश्त नहीं होती थी फिर वहां कैसे रह पाते होंगे रे !’’ दादी उड़ी-उड़ी–सी आसमान की ओर ताकने लगतीं, ‘‘कहते हैं राकस टाट के चीथड़े पहनने को देते हैं। बीमार होने पर दवा नहीं ....मरने पर दो लकड़ियाँ....हाथ भर कफ़न तक नहीं.. तेरे दादा जी उस सर्दी में कैसे रहते होंगे ...?’’ दादी फूटफूटकर रो पड़तीं तो उसे वे समझाते, ‘‘वहां सर्दी नहीं पड़ती दादी बारहों महीने खूब गरमी रहती है.....।’’
पर उस सारे दिन वह अपनी फटी धोती के चाल से आँखों पोंछती रहतीं।
अपने पूजा के देवताओं के पास रखे दादाजी के एक धुँधले-से चित्र पर रोज फूल चढ़ातीं। अक्षत बिखेरतीं। जब तक जिन्दा रहीं उनका यही नेम-नियम रहा।
‘‘हरिकशन कोई चिट्ठी-पतरी नहीं आयी - ?’’ वह सहसा कुछ याद आने पर कहतीं, ‘‘कहते हैं बरस भर में एक ही चिट्ठी भेजने देते हैं। एक ही पाने ! कौन जाने डाकखाने की गड़बड़ में कहीं इधरःउधर न हो गयी हो !’’
पिताजी चुप लगा जाते। क्या उत्तर दें, उन्हें कुछ सूझता न था।
दादी के प्राण दादा जी में बसते थे।
कहते हैं- दादाजी जब ऊन और घोड़ों का व्यापार करने जौलजीबी की तरफ, भोट-तिब्बत की सरहद तक जाते, तब दादी का सारा ध्यान ऊनी कम्बलों, थुलमों भोटिया घोड़ों की खरीद–फरोख्त तक सीमित रहता। दिन-रात वह ऊन और घोड़ों की ही बातें करतीं। पर बाद में दादाजी के क्रान्तिकारी बनने पर उनकी चिन्ताओं के विषय भी बदल गये थे।
-कहते हैं फिरंगी गाय का माँस खाते हैं !
- फिरंगी हमारा धरम-भ्रष्ट करने सात समुन्दर पार से यहां आये हैं।
-अब लड़ाई होगी अपना धरम छोड़ने से तो मर जाना अच्छा है रे ! तब वह छोटा था। दादी की बातें समझ में न आने पर भी वे अबोध परियों और राक्षसों की कहानी जैसी रोचक लगतीं।
जाड़ों की पीली-पीली गुनगुनी धूप में कभी बाहर आँगन में बैठते, या बाहर बर्फ गिरने पर घर के भीतर लोहे के सगड़ की आग के चारों ओर घेरा बनाकर आग सेंकते तो दादी खोयी-खोयी-सी कहतीं-
‘‘तुम्हारे दादाजी को जब जनम-कैद की सजा हुई तो मेरी उमर बीस की थी। तुम्हारा बाप हरिकिशन गोदी का बच्चा था.... तुम्हारे दादा जी को कालापानी ले जाते समय बेड़िया भी लगवायीं, तब माता की जै-जैकार से आकाश गूंज उठा था। आदमियों का कैसा गिरदम्म-सा मच गया था ! इत्ती भीड़ शायद लोगों ने कभी नहीं देखी हो !...
‘‘पर रात को मातम-सा छा गया उस दिन ! आस-पास के सारे गाँव-घरों में कहीं चूल्हा नहीं जला था। मन्दिर की धूनी रात भर धधकती रही थी सैकड़ों लोग आग चारों ओर बैठे रहे....।
पर यहां आकर वह एक तरह से गूँगा-सा क्यों हो गया है ?
अचरज भरी निगाहों से वह चारों ओर देखता है- हर रोज उमड़ते-घुमड़ते काले बादलों को। चारों दिशाओं में बिखरे जल, जल-ही-जल को। अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो, जब बादल न घिरे हों, न गरजे हों, न बरसे हों। थोड़ी-सी झड़ी के बाद फिर एकाएक साफ आसमान। धुली धरती। ठीक सिर पर टकराती चुभती हुई उजली धूप !
अथाह पानी में तैरती-सी हरियाली की हरी-हरी क्यारियाँ ! दूर-दूर तक छिटके छोटे-छोटे द्वीप ! सामने वाला राँस द्वीप तो ऐसा लगता, जैसे हाथ बढ़ाकर छू लेगा ....
वह घण्टों विस्फारित नेत्रों से उन्हें निहारता, न जाने क्या-क्या सोचता रहता है ! परछाइयों की तरह कई आकृतियाँ उभरती-मिटती हैं। स्याह-सफेद कई-कई चित्र !
निर्जन -से इन द्वीपों में से उसे अजनबीपन के साथ-साथ कहीं अपनेपन का कोई अदृश्य रिश्ता-सा भी लगता है।
धरती के कण-कण से एक अव्यक्त गहरा आत्मभाव !
एक लम्बी निःश्वास के साथ, वह आँखें मूँद लेता है।
सच, तब कितना भयानक होगा, वहाँ का वातावरण ! कल रात देर तक वह उस जेट्टी के पास खड़ा रहा। जहाँ कलकत्ता से आनेवाले जलपोत रुका करते थे। कभी ऐसे ही एक जहाज से... एक दिन....ऐसे ही.....इसी तरह....
जब तक दादी जिन्दा थीं, बहकी-बहकी-सी कितनी बातें बतलाया करती थीं, जैसे आँखों देखा हाल सुना रही हों। ‘‘कालापानी में आकाश को छूते भयानक जंगल होते हैं रे ! जंगल–ही-जंगल ! साँपों, बिच्छुओं, जहरीले कीड़े-मकोड़ों से भरे ! जिनके काटे का आदमी पानी तक नहीं माँगता......वनों में खूँख्वार वन-मानुष, तीर-भाले चलाते हैं। आदमियों को भूनकर खा जाते हैं..... बिछौने पर, छतों की शहतीरों पर रस्सी की तरह साँप सरकते रहते हैं। धूल के कणों की तरह बारीक सफेद चींटियाँ देखते-देखते हाथी भी हजम कर जाती हैं।’’
अनपढ़ दादी को, जो जिन्दगी भर अपने गाँव से बाहर नहीं गयी, ये रोमांचक रहस्यपूर्ण बातें कहाँ से मालूम पड़ीं, पता नहीं। कहते हैं, पास के गाँव का एक लड़का अभी भागकर कलकत्ता गया था। वहाँ पुलिस में भर्ती हो गया था। कैदियों को लाने-ले-जाने के काम से दो-तीन बार कालापानी तक हो आया था। हो सकता है लौटकर उसी ने सुनायी हों ये बातें !
दादी कभी-कभी स्वयं से बड़बड़ातीं, ‘‘नाश हो इनका ! कहते हैं ये राकस गोरे, कैदियों की नंगी पीठ पर चाबुक मारते हैं। खाल उधेड़ देते हैं। शरीर लहूलुहान हो जाता है।... दिन–रात बरखा-घाम में भी काम ही काम, पर खाने को दो रूखी रोटियाँ तक नहीं.... तेरे दादाजी से तो भूख कतई बरदाश्त नहीं होती थी फिर वहां कैसे रह पाते होंगे रे !’’ दादी उड़ी-उड़ी–सी आसमान की ओर ताकने लगतीं, ‘‘कहते हैं राकस टाट के चीथड़े पहनने को देते हैं। बीमार होने पर दवा नहीं ....मरने पर दो लकड़ियाँ....हाथ भर कफ़न तक नहीं.. तेरे दादा जी उस सर्दी में कैसे रहते होंगे ...?’’ दादी फूटफूटकर रो पड़तीं तो उसे वे समझाते, ‘‘वहां सर्दी नहीं पड़ती दादी बारहों महीने खूब गरमी रहती है.....।’’
पर उस सारे दिन वह अपनी फटी धोती के चाल से आँखों पोंछती रहतीं।
अपने पूजा के देवताओं के पास रखे दादाजी के एक धुँधले-से चित्र पर रोज फूल चढ़ातीं। अक्षत बिखेरतीं। जब तक जिन्दा रहीं उनका यही नेम-नियम रहा।
‘‘हरिकशन कोई चिट्ठी-पतरी नहीं आयी - ?’’ वह सहसा कुछ याद आने पर कहतीं, ‘‘कहते हैं बरस भर में एक ही चिट्ठी भेजने देते हैं। एक ही पाने ! कौन जाने डाकखाने की गड़बड़ में कहीं इधरःउधर न हो गयी हो !’’
पिताजी चुप लगा जाते। क्या उत्तर दें, उन्हें कुछ सूझता न था।
दादी के प्राण दादा जी में बसते थे।
कहते हैं- दादाजी जब ऊन और घोड़ों का व्यापार करने जौलजीबी की तरफ, भोट-तिब्बत की सरहद तक जाते, तब दादी का सारा ध्यान ऊनी कम्बलों, थुलमों भोटिया घोड़ों की खरीद–फरोख्त तक सीमित रहता। दिन-रात वह ऊन और घोड़ों की ही बातें करतीं। पर बाद में दादाजी के क्रान्तिकारी बनने पर उनकी चिन्ताओं के विषय भी बदल गये थे।
-कहते हैं फिरंगी गाय का माँस खाते हैं !
- फिरंगी हमारा धरम-भ्रष्ट करने सात समुन्दर पार से यहां आये हैं।
-अब लड़ाई होगी अपना धरम छोड़ने से तो मर जाना अच्छा है रे ! तब वह छोटा था। दादी की बातें समझ में न आने पर भी वे अबोध परियों और राक्षसों की कहानी जैसी रोचक लगतीं।
जाड़ों की पीली-पीली गुनगुनी धूप में कभी बाहर आँगन में बैठते, या बाहर बर्फ गिरने पर घर के भीतर लोहे के सगड़ की आग के चारों ओर घेरा बनाकर आग सेंकते तो दादी खोयी-खोयी-सी कहतीं-
‘‘तुम्हारे दादाजी को जब जनम-कैद की सजा हुई तो मेरी उमर बीस की थी। तुम्हारा बाप हरिकिशन गोदी का बच्चा था.... तुम्हारे दादा जी को कालापानी ले जाते समय बेड़िया भी लगवायीं, तब माता की जै-जैकार से आकाश गूंज उठा था। आदमियों का कैसा गिरदम्म-सा मच गया था ! इत्ती भीड़ शायद लोगों ने कभी नहीं देखी हो !...
‘‘पर रात को मातम-सा छा गया उस दिन ! आस-पास के सारे गाँव-घरों में कहीं चूल्हा नहीं जला था। मन्दिर की धूनी रात भर धधकती रही थी सैकड़ों लोग आग चारों ओर बैठे रहे....।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i