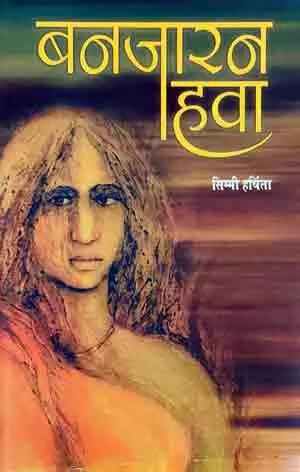|
कहानी संग्रह >> बनजारन हवा बनजारन हवासिम्मी हर्षिता
|
26 पाठक हैं |
|||||||
नारी जीवन की विवशताओं और विडंबनाओं तथा नारी मन के अंतर्द्वंद्वों का चित्रण
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
सुपरिचित कथा लेखिका सिम्मी हर्षिता की मनोविज्ञान प्रधान, मर्मस्पर्शी
कहानियों का पठनीय-संग्रहणीय संकलन। नारी जीवन की विवशताओं और विडंबनाओं
तथा नारी मन के अंतर्द्वद्वों का बेहद बेबाकी से चित्रण करने वाली ये
कहानियाँ नारी की आकांक्षाओं के साथ-साथ उसके विद्रोही स्वरूप का भी
उद्घाटन करतीं हैं।
इन कहानियों में आप पायेंगे समकालीन जीवन के विरोधाभास, छलनापूर्ण संबंधों के दुष्चक्र से टूटते सनातन मानवीय मूल्य, भंग होती आस्थाएं और विश्वास। ये कहानियाँ बेहद पारिवारिक भी हैं। इनमें व्यक्त पीड़ा यदि आपको व्यथित करती है तो इसके साथ साथ झकझोरती भी है।
सिर्फ हवा बनजारन नहीं होती; लेखन शैली भी होती है और उसी का हमें इंतजार रहता है। जैसे हवा तभी ताज़ा रह सकती है जब रुख़ बदल बदल कर बहे, वैसे ही कहानियाँ भी तभी प्रभावशाली हो सकती हैं जब कोई नया रुख़ उजागर करें। यूं भी कहानी संग्रह पढ़ने का मजा़, हवा पर सवार हो कर घूमने की तरह है। ऐसी हवा, जो विभिन्न रूपों-रंगों-तापमानों के दृश्यों पर होकर गुज़रे; उन पर पड़ी धूल की परतें झाड़ कर उन्हें पारदर्शी बनाये और पाठक से यह अपेक्षा रखे कि वह उन्हें अपनी नज़र से नहीं, किसी और की खानाबदोश नज़र से देखेगा।
दृश्य-बिंबों को एक धागे में ऐसे पिरोये कि धागा दिखे तक नहीं। सिम्मी हर्षिता का ‘बनजारन हवा’ एक ऐसा ही पठनीय कहानी संग्रह है, जिस पर बातचीत की जानी ज़रूरी है।
संग्रह की काफ़ी कहानियां, निहायत प्राकृत, पुरअसर और शोख तरीक़े से हमें यह अहसास करवाती हैं कि हमारे समाज में लड़की के लिए बनजारन फ़ितरत को निभाना कितना मुश्किल है। पर जब ‘बनजारन हवा’ कहानी इसी अहसास को कथ्य बनाती है तो असर बढ़ता नहीं, कम हो जाता है।
मेरा क़यास है कि ‘बनजारन हवा’ कहानी का नाम ज़्यादा लोगों की ज़बान पर आयेगा और वह मेरी स्थापना का सबूत होगा। क्योंकि यह कहानी, संग्रह की अन्य कहानियों से पैदा हुए तेज़ हवा के दबाव से हमें मुक्ति दिलाती है; इसलिए उसका नाम, बिना खतरा उठाये, आसानी से मुंह पर आ जाता है। संग्रह में लेखकीय कौशल के ऐसे गतिरोध कुछ और भी मिलेंगे पर वे उसकी शोखी और मौलिकता भरी रफ़्तार को बहुत ज़्यादा रोके नहीं रख पाते। ‘बनजारन हवा’ उन कहानी संग्रहों में से है, जिसे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अपना मनोबल बनाये रखने के लिए भी कि हमारे पास ऐसे लेखक भी हैं, जो बरसों से चुपचाप लिखते आये हैं और अब तक हवा पर सवार होने का साहस बनाये हुए हैं।
इन कहानियों में आप पायेंगे समकालीन जीवन के विरोधाभास, छलनापूर्ण संबंधों के दुष्चक्र से टूटते सनातन मानवीय मूल्य, भंग होती आस्थाएं और विश्वास। ये कहानियाँ बेहद पारिवारिक भी हैं। इनमें व्यक्त पीड़ा यदि आपको व्यथित करती है तो इसके साथ साथ झकझोरती भी है।
सिर्फ हवा बनजारन नहीं होती; लेखन शैली भी होती है और उसी का हमें इंतजार रहता है। जैसे हवा तभी ताज़ा रह सकती है जब रुख़ बदल बदल कर बहे, वैसे ही कहानियाँ भी तभी प्रभावशाली हो सकती हैं जब कोई नया रुख़ उजागर करें। यूं भी कहानी संग्रह पढ़ने का मजा़, हवा पर सवार हो कर घूमने की तरह है। ऐसी हवा, जो विभिन्न रूपों-रंगों-तापमानों के दृश्यों पर होकर गुज़रे; उन पर पड़ी धूल की परतें झाड़ कर उन्हें पारदर्शी बनाये और पाठक से यह अपेक्षा रखे कि वह उन्हें अपनी नज़र से नहीं, किसी और की खानाबदोश नज़र से देखेगा।
दृश्य-बिंबों को एक धागे में ऐसे पिरोये कि धागा दिखे तक नहीं। सिम्मी हर्षिता का ‘बनजारन हवा’ एक ऐसा ही पठनीय कहानी संग्रह है, जिस पर बातचीत की जानी ज़रूरी है।
संग्रह की काफ़ी कहानियां, निहायत प्राकृत, पुरअसर और शोख तरीक़े से हमें यह अहसास करवाती हैं कि हमारे समाज में लड़की के लिए बनजारन फ़ितरत को निभाना कितना मुश्किल है। पर जब ‘बनजारन हवा’ कहानी इसी अहसास को कथ्य बनाती है तो असर बढ़ता नहीं, कम हो जाता है।
मेरा क़यास है कि ‘बनजारन हवा’ कहानी का नाम ज़्यादा लोगों की ज़बान पर आयेगा और वह मेरी स्थापना का सबूत होगा। क्योंकि यह कहानी, संग्रह की अन्य कहानियों से पैदा हुए तेज़ हवा के दबाव से हमें मुक्ति दिलाती है; इसलिए उसका नाम, बिना खतरा उठाये, आसानी से मुंह पर आ जाता है। संग्रह में लेखकीय कौशल के ऐसे गतिरोध कुछ और भी मिलेंगे पर वे उसकी शोखी और मौलिकता भरी रफ़्तार को बहुत ज़्यादा रोके नहीं रख पाते। ‘बनजारन हवा’ उन कहानी संग्रहों में से है, जिसे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अपना मनोबल बनाये रखने के लिए भी कि हमारे पास ऐसे लेखक भी हैं, जो बरसों से चुपचाप लिखते आये हैं और अब तक हवा पर सवार होने का साहस बनाये हुए हैं।
मृदुला गर्ग
(राष्ट्रीय सहारा)
(राष्ट्रीय सहारा)
बनजारन हवा
‘‘आज घर से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है
?’’
‘‘आज ही तो ज़रूरत है।’’
‘‘मतलब ?’’
‘‘पहले तो नौकरी के लिए आवेदन-पत्र मंगवाते थे, पर आज ऐसा विज्ञापन छपा है जो खुद आने को कहता है। क्या पता वहां पहुंचते ही नौकरी मिल जाये।’’
‘‘आज नौकरी के बारे में न सोचकर उसके बारे में सोचो जो तुम्हें देखने आ रहा है। आज तुम्हारा बाहर धूल-धूप में भटकना ठीक नहीं।’’
‘‘ठीक हैं।’’
‘‘तो नहीं जा रही न ?’’
‘‘बस गयी और आयी।’’
‘नानी से लेकर दादी तक के सारे रिश्तेदार इसी शहर की गोद से खुमी की तरह निकले हैं और किसी पुराने पेड़ की जड़ों की तरह इससे चिपके हुए फैलते चले जा रहे हैं। ऐसा है उनका प्यार,’ अपने इस शहर से बाहर जाना हमें तो मौत जैसा लगता है।’ एक ही शहर में एक से परिचितों-रिश्तों के बीच सारी जिंदगी गुज़ार देना कैसा बेढब विचार है। उनके इस मोह के कारण ही सरकार को अपने इस शहर का दायरा बार-बार बड़ा करना पड़ रहा है।
आभा के प्रति चिंतामुक्त होने के बाद गठरी की तरह बांध-बूंध देने वाली मां-बाप की ममता आज से मेरे लिए भी इसी शहर में से एक पतिया-अतिया की तलाश की खुशी में है। एक पतिराम भी कटोरी में दही की तरह जमा हुआ मिलने वाला है। यह कैसा तो एक गावदी विचार है। हरपल इस आकस्मिक दुर्घटना की चिंता मेरे आसपास मंडराती रहती है। अभी वह हादसा हुआ कि हुआ, अभी वह बौड़म आया कि आया, मेरे जीवन को सदैव के लिए इस शहर के कुएं में फेंक देने के लिए, यहां से बाहर जाने की सारी संभावनाएं सदा के लिए खत्म कर देने के लिए।
ओह ! कैसा एकदम गोंदीली जीवन है, हर वक्त आलमारी में बंद पढ़ी-अपढ़ी रहने वाली पुस्तकों की तरह। कहीं कोई दूरी नहीं तय करने को, कोई पहाड़ नहीं पार करने को, नदी नहीं लांघने को, समुद्र नहीं तैरने को। जहाज और रेलगाड़ी का आविष्कार जैसे मेरे लिए न हुआ हो। न गाड़ी मिली, न छूटी न स्टेशन की भाग दौड़ और शोर के भागीदार हुए, न किसी ने हाथ हिलाकर विदा दी, न हम किसी से विदा के दुःख-सुख में अंसुआए, न कोई हमसे दूर गया, न हम किसी के पास आये न दूरी ने यादों के जलतरंग को जन्म दिया, न किसी ने खत लिखने को रंग दिया। न खत लिखना सीखने की कला हमारे किसी काम आयी, न कभी डाकिये को हमारा नाम- पता ढूंढ़ने की याद आयी। जीवन एक तयशुदा समयसारिणी। मेरे पास सारा संसार है भूगोल के नक्शों और ग्लोब में। बस सब कुछ चिप्पू सा खेत में पसरा पड़ा लता से लटका-सटका मुटियाता कद्दू।
गति के लिए घड़कनों में हर पल एक आकुलता धमाचौकड़ी मचाये रहती है। मीलों दूर से सागर कहता है, ‘मै खारा हूं।’ मैं नहीं मानती तो वह उफन उठता है। पर्वत कहता है, मेरी ढलवां चोटियों पर पानी दौड़ते-दौड़ते ठिठक और निठुर जाता है। मैं नहीं विश्वासती तो वह एक पत्थर मेरी ओर फेंक देता है। क्या छोटी-सी बचकानी गिनती में समा जाने योग्य है इस विराटता के सारे आश्चर्य ? मैं समेट लेना चाहती हूं इसकी असीमता को अपनी दृष्टि के सीमांत में और खोज लेना चाहती हूं कोई नव्यता।
कुछ पूर्वजों की विरासत ने, कुछ बुजुर्गों की सीख-सिखावन और रुकावट टुकावट ने, कुछ संगी-साथियों की बतकहियों ने, कुछ छापेखाने ने, कुछ फिल्मों रेडियो और दूरदर्शन ने गा बजा दिया। कुछ वह चुगद बता देगा। रहा-सहा उसकी संतानें और बहु-बेटियां बता देंगी तथा शेष यमराज जी बता देंगे। पर मैंने अपने-आपको क्या बताया ? क्या खोजा और क्या पाया ?
काश ! मेरी जिंदगी होती एक बनजारन हवा। दिन- रात गति में गुम जीवन एक से दूसरे दीप-अदीप में डोलता हुआ भय-अभय से दूर। मेरा विश्राम हर समय बिस्तरबंद बना रहता और कदम किसी अपरिचित राह पर चलते-भटकते अनजाना-अनदेखा तलाशते रहते। पर अपना यह जीवन तो है नकेल में बंधा एक ऊंट, अपनी छोटी-चपटी-सी दुम से मक्खियां उड़ाता हुआ ऊंट, आराम-विराम से जुगाली करता हुआ ऊंट, जाने- पहचाने रेगिस्तान को आंखें बंद किये हुए ऊंघता-सा पार करता हुआ ऊंट पूरी हिफाजत और सावधानी से अपने अंदर पानी और भोजन भरकर एक-एक कदम नाप तौल कर चलता हुआ ऊंट, आसपास से निकलती किसी तेज सवारी की दहशत-वहशत से रुक-ठहर जाने वाला ऊंट, एक बार बैठकर जुगाली करने में लग गया तो फिर जल्दी ही न उठने वाला ऊंट, जिसकी हर करवट का मुझे पता रहता है और जिसकी कोई कल टेढी नहीं।
मैं तो हूं एक घोड़ा जिसकी आंखों पर चढ़ा है दोनों ओर पट्टा चौड़ा ताकि सामने की सड़क को ही केवल देखूं और कहीं इधर-उधर न रेखूं-पेखूं।
सब कुछ कितना निरर्थक और नीरस, कितना उकताहट और सुस्ताहट का मारा हुआ। दीवारों-तारों से घिरा वरदी पहने, कोर्सी किताबें और खाने का डिब्बा बैग में रखे, पानी की बोतल कंधे पर लटकाए, किसी हिफाजत की अंगुली पकड़े स्कूली बच्चा मेरा अस्तित्व। हर पल मेरे मन में ये स्कूली दीवारें फलांगने की अड़ समायी रहती है। लगता है, अनजाने शांत-संतुष्ट आज्ञाकारी दिन बीत गये हैं और अब हर हाल में अंशात-अनींदे-अवसादित रहना है-तभी जग की वजह से, कभी मन के जगराते की वजह से, कभी पायी हुई तृप्ति की वजह से, कभी पायी हुई अतृप्ति की वजह से। कभी उदासी की कब्र खोदते रहना है, कभी खट्टे अंगूरों के लिए उछलते रहना है। जो चाहना है, उसे पाना नहीं-और जो पाना है, उसे चाहना नहीं।
इधर एक बीमारी हो गयी है चलने की। जैसे ही घर से एकाएक कहीं लापता हो जाने का विचार कौंध मारता है, अवसाद भरी गठरी का बोझ धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है और बदरंग मन जगमगा उठता है। शिथिलता का पत्थर टूट जाता है, अटपटे निषेधक विचारों के जाले झड़ जाते हैं, एक स्फूर्ति और खुशी लबालब भर जाती है। खेलता-दौड़ता उत्सवी मनोभाव लौट आता है और तब लगता है कि जीवन केवल पपडियायी मिट्टी ही नहीं है। वह है ऐसा जल, जिसमें हमेशा आकाश झिलमिला सकता है और अपना रंग घोल सकता है।
आज फिर मेरे पैर सैंडिल में धंस गये हैं और पैदल सड़क-दर-सड़क सटर-सटर करने लगे हैं। लापता होने के लिए भला चाहिए भी क्या ? कदम और कदमों के लिए कैसी भी जमीन।
कदम और सड़क पग और पगडंडी...। एक पथ पर कितने पथ-पैदल पथ पार पथ कार पथ भूमिगत पथ। एक पथ पर कितने निषेध ‘शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ’, ‘सावधान आपकी गति पर नजर रखी जा रही है। ‘वक्रगति से गाड़ी चलाने का दंड पांच सौ रुपये’, ‘छेड़छाड़ पर ससुराल जाने का दंड’, लेन ड्राइविंग इज सेन ड्राइविंग’, ‘नरक में जाने की जल्दी मत करो’ सुरक्षा को जीओ और दूसरों को जीवित रहने दो।
राह में एक बाग़, बाग़ में एक बेंच, हिलते-डुलते पत्तों की छाया, हरियाली सूखे पत्तों की दुपकाहट और मैं। नीचे पड़ा हुआ एक कागज बेचैनी से इधर-उधर फड़फड़ा रहा है। न जाने क्यों ? जैसे ही मैं उसे उठाती हूं, वह टकराने लगता है शब्दों के आंसू:
जिस बगिया में बच्चियां नहीं खेल सकतीं निर्भय उन्मुक्त हवा में
जिस आंगन में मुन्नू नहीं जी सकती वांछित होकर
वह बगिया और आंगन जीने योग्य कैसे हो सकते हैं ?
जो संसार बच्चों का बचपन छीन लेता है पेट की भूख के कारण
जो संसार मासूम की मासूमियत चीथ देता है तन के वहशीपन के कारण
वह संसार जीने योग्य कैसे हो सकता है ?
जिन घरों के घेरे में रिश्तों की पवित्र दीवारें ढह जाती हैं
वे रिश्ते और घर जीने योग्य कैसे हो सकते हैं ?
जहां कांटों में फूल हंस न पायें
वे कांटे जीने योग्य कैसे हो सकते हैं ?
ओह ! यह जगह तो बहुत उदासी देती है। चलो कहीं और।
राह में बिछी एक नहर...नहर का किनारा...पीपल का घनेरा पेड़ पानी में मछलियों का खेल लिखे हुए अनेक निर्देश ‘यहां तैरना मना है’, ‘यहां डूबना मना है’, ‘यहां मछली पकड़ना मना है।’ कंकड़-पत्थरों के साथ उदासी-नाराज़गी और आने वाले उस कनतूतर को पानी में फेंककर लौट आना।
गगनचुंबी इमारत की सीढ़ियां चढ़ते-चढ़ते ऊपर पहुंच जाना कहीं पहुंचने के लिए नहीं, कूदने के लिए नहीं। आकाश की निकटता को अनुभव करना, अपने अंतस में मुक्त हवा को भरना, उस बजरबट्टू को ऊपर से नीचे धकेलकर उतर आना।
रेलवे स्टेशन नन्हीं पटरियों पर सरकती लहराती चीखती विशाल रेलगाड़ियां चढ़ने उतरने का एक साथ होता घमासान युद्ध। बिना टिकट सफरना है अपराध। लोग खेलते हैं रोज यह खेल जब तक पकड़े नहीं जाते। मैं भी खेल रही हूं इक खेल घर की पकड़ से दूर। पुल पर से उस हुड़कलचुल्लू को नीचे गिराकर लौट आना।
क़दम..... सड़क... सड़क पर चलती बातों के कदम-‘इधर से आओ’, ‘बात बनी नहीं, ‘अरे जूता मारो उसे’ खों-खों पों-पों ‘अटपट साला।’ सटाक से गिरता पानी का परनाला। ‘नाक कान छिदवा लो...काम साफ करवा लो’..‘फ्लश साफ़ करवा लो।’
चलते चले जाना और कहीं न पहुंचना या कहीं न पहुंचने के लिए चलते जाना...
चलते-चलते भूख का पौधा उग आया है, धीरे-धीरे बढ़ने-खिलने लगा है और उस पर घर कद्दू की तरह उग आया है अपनी हिफ़ाजत अनुशासन और सुरक्षा का झंडा-डंडा हिलाते हुए। भूख को भुट्टा थमा दिया है। भुट्टा घर दादा की तरह बोला छिः ! यूं सड़क चलते हुए भुट्टा खाती हो ?’ मैंने उसे दांतों से काट खाया। वह रोने लगा और मैंने तमाशा देखती भीड़ में अपने को शामिल कर दिया है।
सांप जो ज़हर है, सांप जो मौत है, इस समय दिलबहलाव और रोज़ी-रोटी बना हुआ है। लोग सांप को देख रहे हैं, मैं सपेरे को देख रही हूं। सांप की तरह चमकीली उसकी आँखें उसका सांवला चमकीला शरीर, उसकी चमकीली पीली बीन, बीन पर चिकने चितकबरे सांप और सपेरे का लहराना। मैं सपेरे को देख रही हूं, उसके हाव-भाव को देख रही हूं। एकाएक लगा, मैं उसकी पुरुषीय सर्पीली दृष्टि के घेरे में आ गयी हूं, वह एकटम मुझे देख रहा है, देखे ही जा रहा है और बीन बजाता लहराता जा रहा है बिलकुल मेरे सामने आकर....। मैं आँखें और मुंडी इधर-उधर घुमाते हुए उस पर यह जाहिर करना चाहती हूं- मैं तुम्हें थोड़े ही देख रही हूं। उन असहज लहरों में फिर एक पल को भी ठहर पाना संभव नहीं हो पाता। डर और घबराहट में वहां से चल देती हूं। ओह। सपेरे की वे चिकनी-चमकीली आंखें, सांप-जैसी।
अरे वह घर दादा तो यहां भी मेरा पीछा कर रहा है अपने उपदेसों से, ‘अरी ओ ! सोच संभल कर चल, यूं न भटक सड़कों-गलियों में, अनदेखा। कर पुरुषों की नज़रों को अनसुना कर उनके फ़िक़रों को और मेरी सुरक्षा में आ जा। क्या यह सब तुझे शोभा देता है किसी पुरुष के हावों-भावों को पढ़ना ? तेरे मां-पा तैयारी में जुटे हैं उस महाअथिति और परीक्षक निरीक्षक के स्वागत में। घर को सजाया-संवारा जा रहा है। लो, रसगुल्ले और बर्फी भी आ गयी है। लो, तुम्हारी बहना आभा भी आ गयी है तुम्हें ठीक से सजाने-संवारने के लिए ताकि वह तुम्हें देखते ही मुस्करा दे।
मिल्क बूथ के अंदर बैठी दो लडकियां। बाहर पंक्ति बनाती-तोड़ती भीड़...भीड़ को अनुशासन में रखता डंडा थामे सीकिया पुलिसमैन...खिड़की के अंदर से झांकती दो जोड़ी चंचल आंखें। खाली बोतलों के लेन-देन के साथ किशोर युवा मुस्कानों का आदान-प्रदान थमने को नहीं आ रहा। कुछ देर वह खेल देखने के बाद एक चक्कर मैं पिछवाड़े में भी लगा आती हूं। एक लड़की संशयात्मक व्यग्रता से मेरी ओर देखती है और चौकस आवाज़ में साथ वाली लड़की से कहती है, ‘‘पता नहीं ये कौन और कैसी लड़की है ? कितनी देर से यहां खड़ी हमारे पीछे पड़ी है।’’
‘चलो छोड़ो यह घूरती गुप्तचरी वाली बोड़हा हरकतें। किसी को यूं शंका-कुशंका में डालकर परेशान करना क्या कोई अच्छी बात है ? लोग यातायात को सहज भाव से लेते हैं, पर ट्रैफिक जाम से घबराते हैं। सो अपनी गाड़ी स्टार्ट करो अब।’’
एक बारात चली जा रही है, खूब रौनक़ और धूमधाम से। तृप्ता से जब कहो, ‘देखो बारात जा रही है।’ तो बेसुरेपन से कहती है, जब एक बार अपनी बारात और उसका नतीजा देख लिया हो तो फिर बारात देखने की इच्छा नहीं रहती। बारात का मतलब है बेढब जिम्मेवारियों और रिश्तों के चक्रव्यूह का आजन्म कारावास।’
याद आ जाती है आज की सुबह सुहावनी सी। लगभग सात का समय। एक नवब्याहता नंगे पांव अपने घर के खूंटे से रस्सी तुड़ाकर भाग आयी है। पीछे-पीछे अपने छोटे बेटे का कंधा थामे स्कूटर पर सास, उसके पीछे हवाई चप्पल में घिसटता हुआ खूंटा। उस खूंटे की मालकिन ने आते ही झपटकर बहू को दबोच लिया है। जू़ड़ा उसकी अंगुलियों की पकड़ में है और वह उसे पूरे दम से दायें-बायें मरोड़ खींचकर एक ही सवाल बार-बार दोहरा रही है, बोल, बोल ! कहां जायेगी ? हूं, कहां जायेगी ?’’
वह न खिंचते बाल छुड़ाने की कोशिश करती है, न इधर-उधर से पड़ते चांटों-मुक्कों का विरोध करती है और न उस मंडराते सवाल का जवाब देती है। वह न रोती है मार से और न क्रोधित होती है और न किसी बदले में बहती है। शायद उसने बदला ले ही लिया है घर की दीवारें लांघकर और सबको चौराहे पर ला खड़ा कर। वह शांत और सुरक्षित मनोभाव लिये खड़ी है खुले वातावरण की निगहबानी में। अब जैसे कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
‘‘चल चल वापस !’’ ठेलता-धकियाता हुआ आदेश।
वह वापस भी नहीं चलती। पक्का मुंह बनाये नंगे पांवों से धरती पर जस-की-तस ठस खड़ी रहती है, गालियां सुनती रहती है, मार खाती रहती है, अंगूठे से जमीन कुरेदती रहती है जैसे कि वह उससे ही अपनी दुःखबीती कह रही हो।
कोई राह चलता बुजुर्ग उसे समझाता है, जाओ बेटी, अपने घर जाओ।’’
वह निर्विकार अनसुना चेहरा लिये खड़ी रहती है। लोग उत्सुकता से रुकते हैं, देखते हैं, उसकी मेहंदी-तिल्ला-गोटा और चूड़ा और चले जाते हैं। सास जब मार-खींचकर, गाली-गलौज कर थक जाती है तो हांफने लगती है, तेज़ी से धड़कता दिल थामकर सड़क से लगे पैदल पथ पर बैठ जाती है और हाल बेहाल-सी पसीना पोंछने लगती है। सामने वाले घर से एक महिला हमदर्दी का गिलास ले आती है। उसे पिलाती है और शांत होने के लिए कहती है। शांति की बात सुनकर वह और भी अशांत हो जाती है, पूरी बेचारगी के साथ जोर-जोर से सांस लेने लगती है, आंख नाक पोंछने लगती है। छोटा बेटा फिर स्कूटर पर आता है और मां को घर ले जाता है। पति जो अब तक हवाई चप्पल में घिसटता दूर खड़ा-खड़ा चुपचाप मां के तीरंदाजी करतब भोले बचुए की तरह देख रहा था, अब पत्नी के पास आता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। हर कथन, आग्रह और प्रश्न का एक ही उत्तर आ रहा है, नकार की मौन अड़। सात से आठ-आठ से साढ़े आठ। इस बीच वे चलकर पेड़ की छाया तले आ गये हैं सीधी पड़ती धूप से बचने के लिए। कोई रिश्तेदार आकर खूंटे को कुछ समझाता है। जमी हुई स्थिति में हलचल होती है। वह पत्नी को लेकर बस स्टाप की ओर चल पड़ता है जिस ओर वह घंटे भर से लगातार देख रही थी।
मैं बारात के संग-संग चल पड़ती हूं। एक स्वर दूसरे से पूछता है, ‘‘राधा के क्या हालचाल हैं ?’’
दूसरा स्वर उतराता है, ‘‘उसकी गाय गुम गयी थी। मिल गयी है।’’
दोनों हंस पड़े। ‘‘भई ये हाल तो गाय का है, राधा का नहीं, पहला स्वर बोला।
‘‘स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति का क्या हाल और क्या चाल ! हमसे जुड़ी-तुड़ी चीज़ों का हाल ही तो हमारा हाल-बेहाल बन जाता है। दावा तो बहुत है ‘मैं’ का, पर आख़िर हम हैं क्या ?’’
उसे सुनकर मुझे अपना हालचाल याद आ गया। आज एक उल्लू-पुल्लू शाम को मुझे देखने आने वाला है, पर मैं उसे नहीं देखना चाहती। तब मैं शाम तक क्या करूं ? क्या यूं ही सड़कें नापती चलूं ? उस नौकरी की ही ख़बर क्यों न ले ली जाये ? शायद वह मेरा ही इंतजार कर रही हो। इसी ओर ही तो है वह जगह।
भटकते-चलते मुझे ध्यान आया कि शहर का यह भाग तो शायद मैंने पहले कभी देखा नहीं। इतने बर्षों में भी यह शहर मेरे लिए कितना नया है क्योंकि मैंने इसे कदमों से नापा नहीं। या शायद मेरे दिमाग का नक़्शा ही ऐसा बोदा है कि मुझे व्यक्तियों, जगहों, मकानों और सड़कों के नाम तथा स्थिति ठीक से याद नहीं रहती। हर बार उन्हें नये सिरे से ढूंढ़ना सुलझाना पड़ता है। यहां तो देखे-अनदेखे का अजब घालमेल हो गया है। दारा रोड। शक्करपारा रोड। पर अर्जुन रोड तो कहीं दिखायी नहीं देती। यहीं कहीं तो मैंने देखा था उसे पिछली बार। किसी राहगीर से पूछा तो उसने कहा, ‘‘इधर।’’
मैं इधर भी गयी, उधर भी गयी और अर्जुन रोड के बदले दुर्योधन रोड पर पहुंच गयी। सड़क के एक गोल घेरे से निकलकर दूसरे घेरे में और फिर तीसरे घेरे में। एक तिपहिये वाले से पूछा, ‘‘अर्जुन रोड किधर है ?’’
‘‘आइए, बैठिए,’’ उसने झटपट कहा और मैं सम्मोहित-सी घबरायी सी डूबती सी उतरायी सी उस तिनके पर बैठ गयी।
जब उसने तिपहिया चालू किया तो दिमाग ने प्रश्न, किया, ‘तुमने उससे क्या कहा था ?’
अर्जुन रोड कहां है ?’’
‘‘और उसने क्या कहा ?’
‘‘आइए, बैठिए।’
अरे ये तो मुझे अनाड़ी- कबाड़ी समझकर भगाये लिये जा रहा है।
‘‘अरे स्कूटरवाले, ठहरो तुम कहां लिये जा रहे हो ? तुमसे किसने कहा था अर्जुन रोड चलने को ? उतारो मुझे’’, मैं कहते कहते चिल्ला पड़ी।
‘‘लाइए, पैसे लाइए इतनी दूर के।’’
‘‘कैसे पैसे ? दूर कहां ? अभी ही तो बैठी हूं और अभी ही तो उतर गयी हीं’’, मैं झटपट उतरकर चल दी अटपटाती चाल में।
‘‘पागल लगती है यह लड़की !’’
मुझे इस वाक्य में क्रोध के बदले अपना बचाव नज़र आया। मैं चुप सामने दिखने वाली लंबी काली सड़क को तेज़ी से नापने लगी। एक बार जल्दी में पांव मुड़ गया और चप्पल की तनी टूट गयी। एक बार साड़ी पांव के नीचे आ गयी और गिरते-गिरते बची। पीछे से कार सर्र करती मुझे धूल में रौंदती हुई निकल गयी। स्कूटर वाला आगे से पीछे की ओर तथा फिर पीछे से आगे की ओर थोड़ी-थोड़ी देर बाद निकल जाता कहता हुआ, ‘‘चलो केवल एक रुपये में पहुँचा देता हूं।’’
अरे तो क्या इसने सचमुच ही मुझे पागल समझ लिया है ? एक लसूड़ा घर आ रहा है और कई लसूड़े राह चलते मिल जाते हैं।
मैंने बचाव के लिए भीड़ को इधर-उधर ढूंढा तो दादा ने हांक लगायी, अरी ओर मूर्खा ! तेरे मन की ये फितूरबाजी और सूनी सड़कों पर भटकती करतूतें यदि तेरे मां पा को पता चलें तो वे क्या सोचें ? मत भूल कि एक लड़की है और लड़की को हर कदम पर सावधान रहना पड़ता है।’’
चलो गोली मारो उस साक्षात्कार को, कौन सी वह नौकरी मुझे ही मिलने वाली है ? खुद तो बहुत चल ली, अब क्यों न दूसरों को चलते हुए देखा जाये ? इस जीवन में कुछ और न बन पायें, पर इतने भी गये गुज़रे तो नहीं कि दर्शक भी न बन पायें। यदि दुनिया में दर्शक न होते तो सारे सांस्कृतिक क्रिया-कलाप ठप हो चुके होते। दर्शक जाति की अपनी ही महिमा है जो करोड़ों की फिल्म को एक नज़र में हिट और पिट करती है।
आ हा ! फिल्म का नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। अपने फिल्मी उत्साह की चपेट में जो भी मेरे आसपास होता है, उसे मैं अपने साथ बहा ले जाती हूं। लोगों को उनके ज़रूरी काम बिसरा देती हूं और इनकारी के सारे दरवाज़े- खिड़कियां बंद कर देती हूं।
‘‘आज ही तो ज़रूरत है।’’
‘‘मतलब ?’’
‘‘पहले तो नौकरी के लिए आवेदन-पत्र मंगवाते थे, पर आज ऐसा विज्ञापन छपा है जो खुद आने को कहता है। क्या पता वहां पहुंचते ही नौकरी मिल जाये।’’
‘‘आज नौकरी के बारे में न सोचकर उसके बारे में सोचो जो तुम्हें देखने आ रहा है। आज तुम्हारा बाहर धूल-धूप में भटकना ठीक नहीं।’’
‘‘ठीक हैं।’’
‘‘तो नहीं जा रही न ?’’
‘‘बस गयी और आयी।’’
‘नानी से लेकर दादी तक के सारे रिश्तेदार इसी शहर की गोद से खुमी की तरह निकले हैं और किसी पुराने पेड़ की जड़ों की तरह इससे चिपके हुए फैलते चले जा रहे हैं। ऐसा है उनका प्यार,’ अपने इस शहर से बाहर जाना हमें तो मौत जैसा लगता है।’ एक ही शहर में एक से परिचितों-रिश्तों के बीच सारी जिंदगी गुज़ार देना कैसा बेढब विचार है। उनके इस मोह के कारण ही सरकार को अपने इस शहर का दायरा बार-बार बड़ा करना पड़ रहा है।
आभा के प्रति चिंतामुक्त होने के बाद गठरी की तरह बांध-बूंध देने वाली मां-बाप की ममता आज से मेरे लिए भी इसी शहर में से एक पतिया-अतिया की तलाश की खुशी में है। एक पतिराम भी कटोरी में दही की तरह जमा हुआ मिलने वाला है। यह कैसा तो एक गावदी विचार है। हरपल इस आकस्मिक दुर्घटना की चिंता मेरे आसपास मंडराती रहती है। अभी वह हादसा हुआ कि हुआ, अभी वह बौड़म आया कि आया, मेरे जीवन को सदैव के लिए इस शहर के कुएं में फेंक देने के लिए, यहां से बाहर जाने की सारी संभावनाएं सदा के लिए खत्म कर देने के लिए।
ओह ! कैसा एकदम गोंदीली जीवन है, हर वक्त आलमारी में बंद पढ़ी-अपढ़ी रहने वाली पुस्तकों की तरह। कहीं कोई दूरी नहीं तय करने को, कोई पहाड़ नहीं पार करने को, नदी नहीं लांघने को, समुद्र नहीं तैरने को। जहाज और रेलगाड़ी का आविष्कार जैसे मेरे लिए न हुआ हो। न गाड़ी मिली, न छूटी न स्टेशन की भाग दौड़ और शोर के भागीदार हुए, न किसी ने हाथ हिलाकर विदा दी, न हम किसी से विदा के दुःख-सुख में अंसुआए, न कोई हमसे दूर गया, न हम किसी के पास आये न दूरी ने यादों के जलतरंग को जन्म दिया, न किसी ने खत लिखने को रंग दिया। न खत लिखना सीखने की कला हमारे किसी काम आयी, न कभी डाकिये को हमारा नाम- पता ढूंढ़ने की याद आयी। जीवन एक तयशुदा समयसारिणी। मेरे पास सारा संसार है भूगोल के नक्शों और ग्लोब में। बस सब कुछ चिप्पू सा खेत में पसरा पड़ा लता से लटका-सटका मुटियाता कद्दू।
गति के लिए घड़कनों में हर पल एक आकुलता धमाचौकड़ी मचाये रहती है। मीलों दूर से सागर कहता है, ‘मै खारा हूं।’ मैं नहीं मानती तो वह उफन उठता है। पर्वत कहता है, मेरी ढलवां चोटियों पर पानी दौड़ते-दौड़ते ठिठक और निठुर जाता है। मैं नहीं विश्वासती तो वह एक पत्थर मेरी ओर फेंक देता है। क्या छोटी-सी बचकानी गिनती में समा जाने योग्य है इस विराटता के सारे आश्चर्य ? मैं समेट लेना चाहती हूं इसकी असीमता को अपनी दृष्टि के सीमांत में और खोज लेना चाहती हूं कोई नव्यता।
कुछ पूर्वजों की विरासत ने, कुछ बुजुर्गों की सीख-सिखावन और रुकावट टुकावट ने, कुछ संगी-साथियों की बतकहियों ने, कुछ छापेखाने ने, कुछ फिल्मों रेडियो और दूरदर्शन ने गा बजा दिया। कुछ वह चुगद बता देगा। रहा-सहा उसकी संतानें और बहु-बेटियां बता देंगी तथा शेष यमराज जी बता देंगे। पर मैंने अपने-आपको क्या बताया ? क्या खोजा और क्या पाया ?
काश ! मेरी जिंदगी होती एक बनजारन हवा। दिन- रात गति में गुम जीवन एक से दूसरे दीप-अदीप में डोलता हुआ भय-अभय से दूर। मेरा विश्राम हर समय बिस्तरबंद बना रहता और कदम किसी अपरिचित राह पर चलते-भटकते अनजाना-अनदेखा तलाशते रहते। पर अपना यह जीवन तो है नकेल में बंधा एक ऊंट, अपनी छोटी-चपटी-सी दुम से मक्खियां उड़ाता हुआ ऊंट, आराम-विराम से जुगाली करता हुआ ऊंट, जाने- पहचाने रेगिस्तान को आंखें बंद किये हुए ऊंघता-सा पार करता हुआ ऊंट पूरी हिफाजत और सावधानी से अपने अंदर पानी और भोजन भरकर एक-एक कदम नाप तौल कर चलता हुआ ऊंट, आसपास से निकलती किसी तेज सवारी की दहशत-वहशत से रुक-ठहर जाने वाला ऊंट, एक बार बैठकर जुगाली करने में लग गया तो फिर जल्दी ही न उठने वाला ऊंट, जिसकी हर करवट का मुझे पता रहता है और जिसकी कोई कल टेढी नहीं।
मैं तो हूं एक घोड़ा जिसकी आंखों पर चढ़ा है दोनों ओर पट्टा चौड़ा ताकि सामने की सड़क को ही केवल देखूं और कहीं इधर-उधर न रेखूं-पेखूं।
सब कुछ कितना निरर्थक और नीरस, कितना उकताहट और सुस्ताहट का मारा हुआ। दीवारों-तारों से घिरा वरदी पहने, कोर्सी किताबें और खाने का डिब्बा बैग में रखे, पानी की बोतल कंधे पर लटकाए, किसी हिफाजत की अंगुली पकड़े स्कूली बच्चा मेरा अस्तित्व। हर पल मेरे मन में ये स्कूली दीवारें फलांगने की अड़ समायी रहती है। लगता है, अनजाने शांत-संतुष्ट आज्ञाकारी दिन बीत गये हैं और अब हर हाल में अंशात-अनींदे-अवसादित रहना है-तभी जग की वजह से, कभी मन के जगराते की वजह से, कभी पायी हुई तृप्ति की वजह से, कभी पायी हुई अतृप्ति की वजह से। कभी उदासी की कब्र खोदते रहना है, कभी खट्टे अंगूरों के लिए उछलते रहना है। जो चाहना है, उसे पाना नहीं-और जो पाना है, उसे चाहना नहीं।
इधर एक बीमारी हो गयी है चलने की। जैसे ही घर से एकाएक कहीं लापता हो जाने का विचार कौंध मारता है, अवसाद भरी गठरी का बोझ धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है और बदरंग मन जगमगा उठता है। शिथिलता का पत्थर टूट जाता है, अटपटे निषेधक विचारों के जाले झड़ जाते हैं, एक स्फूर्ति और खुशी लबालब भर जाती है। खेलता-दौड़ता उत्सवी मनोभाव लौट आता है और तब लगता है कि जीवन केवल पपडियायी मिट्टी ही नहीं है। वह है ऐसा जल, जिसमें हमेशा आकाश झिलमिला सकता है और अपना रंग घोल सकता है।
आज फिर मेरे पैर सैंडिल में धंस गये हैं और पैदल सड़क-दर-सड़क सटर-सटर करने लगे हैं। लापता होने के लिए भला चाहिए भी क्या ? कदम और कदमों के लिए कैसी भी जमीन।
कदम और सड़क पग और पगडंडी...। एक पथ पर कितने पथ-पैदल पथ पार पथ कार पथ भूमिगत पथ। एक पथ पर कितने निषेध ‘शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ’, ‘सावधान आपकी गति पर नजर रखी जा रही है। ‘वक्रगति से गाड़ी चलाने का दंड पांच सौ रुपये’, ‘छेड़छाड़ पर ससुराल जाने का दंड’, लेन ड्राइविंग इज सेन ड्राइविंग’, ‘नरक में जाने की जल्दी मत करो’ सुरक्षा को जीओ और दूसरों को जीवित रहने दो।
राह में एक बाग़, बाग़ में एक बेंच, हिलते-डुलते पत्तों की छाया, हरियाली सूखे पत्तों की दुपकाहट और मैं। नीचे पड़ा हुआ एक कागज बेचैनी से इधर-उधर फड़फड़ा रहा है। न जाने क्यों ? जैसे ही मैं उसे उठाती हूं, वह टकराने लगता है शब्दों के आंसू:
जिस बगिया में बच्चियां नहीं खेल सकतीं निर्भय उन्मुक्त हवा में
जिस आंगन में मुन्नू नहीं जी सकती वांछित होकर
वह बगिया और आंगन जीने योग्य कैसे हो सकते हैं ?
जो संसार बच्चों का बचपन छीन लेता है पेट की भूख के कारण
जो संसार मासूम की मासूमियत चीथ देता है तन के वहशीपन के कारण
वह संसार जीने योग्य कैसे हो सकता है ?
जिन घरों के घेरे में रिश्तों की पवित्र दीवारें ढह जाती हैं
वे रिश्ते और घर जीने योग्य कैसे हो सकते हैं ?
जहां कांटों में फूल हंस न पायें
वे कांटे जीने योग्य कैसे हो सकते हैं ?
ओह ! यह जगह तो बहुत उदासी देती है। चलो कहीं और।
राह में बिछी एक नहर...नहर का किनारा...पीपल का घनेरा पेड़ पानी में मछलियों का खेल लिखे हुए अनेक निर्देश ‘यहां तैरना मना है’, ‘यहां डूबना मना है’, ‘यहां मछली पकड़ना मना है।’ कंकड़-पत्थरों के साथ उदासी-नाराज़गी और आने वाले उस कनतूतर को पानी में फेंककर लौट आना।
गगनचुंबी इमारत की सीढ़ियां चढ़ते-चढ़ते ऊपर पहुंच जाना कहीं पहुंचने के लिए नहीं, कूदने के लिए नहीं। आकाश की निकटता को अनुभव करना, अपने अंतस में मुक्त हवा को भरना, उस बजरबट्टू को ऊपर से नीचे धकेलकर उतर आना।
रेलवे स्टेशन नन्हीं पटरियों पर सरकती लहराती चीखती विशाल रेलगाड़ियां चढ़ने उतरने का एक साथ होता घमासान युद्ध। बिना टिकट सफरना है अपराध। लोग खेलते हैं रोज यह खेल जब तक पकड़े नहीं जाते। मैं भी खेल रही हूं इक खेल घर की पकड़ से दूर। पुल पर से उस हुड़कलचुल्लू को नीचे गिराकर लौट आना।
क़दम..... सड़क... सड़क पर चलती बातों के कदम-‘इधर से आओ’, ‘बात बनी नहीं, ‘अरे जूता मारो उसे’ खों-खों पों-पों ‘अटपट साला।’ सटाक से गिरता पानी का परनाला। ‘नाक कान छिदवा लो...काम साफ करवा लो’..‘फ्लश साफ़ करवा लो।’
चलते चले जाना और कहीं न पहुंचना या कहीं न पहुंचने के लिए चलते जाना...
चलते-चलते भूख का पौधा उग आया है, धीरे-धीरे बढ़ने-खिलने लगा है और उस पर घर कद्दू की तरह उग आया है अपनी हिफ़ाजत अनुशासन और सुरक्षा का झंडा-डंडा हिलाते हुए। भूख को भुट्टा थमा दिया है। भुट्टा घर दादा की तरह बोला छिः ! यूं सड़क चलते हुए भुट्टा खाती हो ?’ मैंने उसे दांतों से काट खाया। वह रोने लगा और मैंने तमाशा देखती भीड़ में अपने को शामिल कर दिया है।
सांप जो ज़हर है, सांप जो मौत है, इस समय दिलबहलाव और रोज़ी-रोटी बना हुआ है। लोग सांप को देख रहे हैं, मैं सपेरे को देख रही हूं। सांप की तरह चमकीली उसकी आँखें उसका सांवला चमकीला शरीर, उसकी चमकीली पीली बीन, बीन पर चिकने चितकबरे सांप और सपेरे का लहराना। मैं सपेरे को देख रही हूं, उसके हाव-भाव को देख रही हूं। एकाएक लगा, मैं उसकी पुरुषीय सर्पीली दृष्टि के घेरे में आ गयी हूं, वह एकटम मुझे देख रहा है, देखे ही जा रहा है और बीन बजाता लहराता जा रहा है बिलकुल मेरे सामने आकर....। मैं आँखें और मुंडी इधर-उधर घुमाते हुए उस पर यह जाहिर करना चाहती हूं- मैं तुम्हें थोड़े ही देख रही हूं। उन असहज लहरों में फिर एक पल को भी ठहर पाना संभव नहीं हो पाता। डर और घबराहट में वहां से चल देती हूं। ओह। सपेरे की वे चिकनी-चमकीली आंखें, सांप-जैसी।
अरे वह घर दादा तो यहां भी मेरा पीछा कर रहा है अपने उपदेसों से, ‘अरी ओ ! सोच संभल कर चल, यूं न भटक सड़कों-गलियों में, अनदेखा। कर पुरुषों की नज़रों को अनसुना कर उनके फ़िक़रों को और मेरी सुरक्षा में आ जा। क्या यह सब तुझे शोभा देता है किसी पुरुष के हावों-भावों को पढ़ना ? तेरे मां-पा तैयारी में जुटे हैं उस महाअथिति और परीक्षक निरीक्षक के स्वागत में। घर को सजाया-संवारा जा रहा है। लो, रसगुल्ले और बर्फी भी आ गयी है। लो, तुम्हारी बहना आभा भी आ गयी है तुम्हें ठीक से सजाने-संवारने के लिए ताकि वह तुम्हें देखते ही मुस्करा दे।
मिल्क बूथ के अंदर बैठी दो लडकियां। बाहर पंक्ति बनाती-तोड़ती भीड़...भीड़ को अनुशासन में रखता डंडा थामे सीकिया पुलिसमैन...खिड़की के अंदर से झांकती दो जोड़ी चंचल आंखें। खाली बोतलों के लेन-देन के साथ किशोर युवा मुस्कानों का आदान-प्रदान थमने को नहीं आ रहा। कुछ देर वह खेल देखने के बाद एक चक्कर मैं पिछवाड़े में भी लगा आती हूं। एक लड़की संशयात्मक व्यग्रता से मेरी ओर देखती है और चौकस आवाज़ में साथ वाली लड़की से कहती है, ‘‘पता नहीं ये कौन और कैसी लड़की है ? कितनी देर से यहां खड़ी हमारे पीछे पड़ी है।’’
‘चलो छोड़ो यह घूरती गुप्तचरी वाली बोड़हा हरकतें। किसी को यूं शंका-कुशंका में डालकर परेशान करना क्या कोई अच्छी बात है ? लोग यातायात को सहज भाव से लेते हैं, पर ट्रैफिक जाम से घबराते हैं। सो अपनी गाड़ी स्टार्ट करो अब।’’
एक बारात चली जा रही है, खूब रौनक़ और धूमधाम से। तृप्ता से जब कहो, ‘देखो बारात जा रही है।’ तो बेसुरेपन से कहती है, जब एक बार अपनी बारात और उसका नतीजा देख लिया हो तो फिर बारात देखने की इच्छा नहीं रहती। बारात का मतलब है बेढब जिम्मेवारियों और रिश्तों के चक्रव्यूह का आजन्म कारावास।’
याद आ जाती है आज की सुबह सुहावनी सी। लगभग सात का समय। एक नवब्याहता नंगे पांव अपने घर के खूंटे से रस्सी तुड़ाकर भाग आयी है। पीछे-पीछे अपने छोटे बेटे का कंधा थामे स्कूटर पर सास, उसके पीछे हवाई चप्पल में घिसटता हुआ खूंटा। उस खूंटे की मालकिन ने आते ही झपटकर बहू को दबोच लिया है। जू़ड़ा उसकी अंगुलियों की पकड़ में है और वह उसे पूरे दम से दायें-बायें मरोड़ खींचकर एक ही सवाल बार-बार दोहरा रही है, बोल, बोल ! कहां जायेगी ? हूं, कहां जायेगी ?’’
वह न खिंचते बाल छुड़ाने की कोशिश करती है, न इधर-उधर से पड़ते चांटों-मुक्कों का विरोध करती है और न उस मंडराते सवाल का जवाब देती है। वह न रोती है मार से और न क्रोधित होती है और न किसी बदले में बहती है। शायद उसने बदला ले ही लिया है घर की दीवारें लांघकर और सबको चौराहे पर ला खड़ा कर। वह शांत और सुरक्षित मनोभाव लिये खड़ी है खुले वातावरण की निगहबानी में। अब जैसे कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
‘‘चल चल वापस !’’ ठेलता-धकियाता हुआ आदेश।
वह वापस भी नहीं चलती। पक्का मुंह बनाये नंगे पांवों से धरती पर जस-की-तस ठस खड़ी रहती है, गालियां सुनती रहती है, मार खाती रहती है, अंगूठे से जमीन कुरेदती रहती है जैसे कि वह उससे ही अपनी दुःखबीती कह रही हो।
कोई राह चलता बुजुर्ग उसे समझाता है, जाओ बेटी, अपने घर जाओ।’’
वह निर्विकार अनसुना चेहरा लिये खड़ी रहती है। लोग उत्सुकता से रुकते हैं, देखते हैं, उसकी मेहंदी-तिल्ला-गोटा और चूड़ा और चले जाते हैं। सास जब मार-खींचकर, गाली-गलौज कर थक जाती है तो हांफने लगती है, तेज़ी से धड़कता दिल थामकर सड़क से लगे पैदल पथ पर बैठ जाती है और हाल बेहाल-सी पसीना पोंछने लगती है। सामने वाले घर से एक महिला हमदर्दी का गिलास ले आती है। उसे पिलाती है और शांत होने के लिए कहती है। शांति की बात सुनकर वह और भी अशांत हो जाती है, पूरी बेचारगी के साथ जोर-जोर से सांस लेने लगती है, आंख नाक पोंछने लगती है। छोटा बेटा फिर स्कूटर पर आता है और मां को घर ले जाता है। पति जो अब तक हवाई चप्पल में घिसटता दूर खड़ा-खड़ा चुपचाप मां के तीरंदाजी करतब भोले बचुए की तरह देख रहा था, अब पत्नी के पास आता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। हर कथन, आग्रह और प्रश्न का एक ही उत्तर आ रहा है, नकार की मौन अड़। सात से आठ-आठ से साढ़े आठ। इस बीच वे चलकर पेड़ की छाया तले आ गये हैं सीधी पड़ती धूप से बचने के लिए। कोई रिश्तेदार आकर खूंटे को कुछ समझाता है। जमी हुई स्थिति में हलचल होती है। वह पत्नी को लेकर बस स्टाप की ओर चल पड़ता है जिस ओर वह घंटे भर से लगातार देख रही थी।
मैं बारात के संग-संग चल पड़ती हूं। एक स्वर दूसरे से पूछता है, ‘‘राधा के क्या हालचाल हैं ?’’
दूसरा स्वर उतराता है, ‘‘उसकी गाय गुम गयी थी। मिल गयी है।’’
दोनों हंस पड़े। ‘‘भई ये हाल तो गाय का है, राधा का नहीं, पहला स्वर बोला।
‘‘स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति का क्या हाल और क्या चाल ! हमसे जुड़ी-तुड़ी चीज़ों का हाल ही तो हमारा हाल-बेहाल बन जाता है। दावा तो बहुत है ‘मैं’ का, पर आख़िर हम हैं क्या ?’’
उसे सुनकर मुझे अपना हालचाल याद आ गया। आज एक उल्लू-पुल्लू शाम को मुझे देखने आने वाला है, पर मैं उसे नहीं देखना चाहती। तब मैं शाम तक क्या करूं ? क्या यूं ही सड़कें नापती चलूं ? उस नौकरी की ही ख़बर क्यों न ले ली जाये ? शायद वह मेरा ही इंतजार कर रही हो। इसी ओर ही तो है वह जगह।
भटकते-चलते मुझे ध्यान आया कि शहर का यह भाग तो शायद मैंने पहले कभी देखा नहीं। इतने बर्षों में भी यह शहर मेरे लिए कितना नया है क्योंकि मैंने इसे कदमों से नापा नहीं। या शायद मेरे दिमाग का नक़्शा ही ऐसा बोदा है कि मुझे व्यक्तियों, जगहों, मकानों और सड़कों के नाम तथा स्थिति ठीक से याद नहीं रहती। हर बार उन्हें नये सिरे से ढूंढ़ना सुलझाना पड़ता है। यहां तो देखे-अनदेखे का अजब घालमेल हो गया है। दारा रोड। शक्करपारा रोड। पर अर्जुन रोड तो कहीं दिखायी नहीं देती। यहीं कहीं तो मैंने देखा था उसे पिछली बार। किसी राहगीर से पूछा तो उसने कहा, ‘‘इधर।’’
मैं इधर भी गयी, उधर भी गयी और अर्जुन रोड के बदले दुर्योधन रोड पर पहुंच गयी। सड़क के एक गोल घेरे से निकलकर दूसरे घेरे में और फिर तीसरे घेरे में। एक तिपहिये वाले से पूछा, ‘‘अर्जुन रोड किधर है ?’’
‘‘आइए, बैठिए,’’ उसने झटपट कहा और मैं सम्मोहित-सी घबरायी सी डूबती सी उतरायी सी उस तिनके पर बैठ गयी।
जब उसने तिपहिया चालू किया तो दिमाग ने प्रश्न, किया, ‘तुमने उससे क्या कहा था ?’
अर्जुन रोड कहां है ?’’
‘‘और उसने क्या कहा ?’
‘‘आइए, बैठिए।’
अरे ये तो मुझे अनाड़ी- कबाड़ी समझकर भगाये लिये जा रहा है।
‘‘अरे स्कूटरवाले, ठहरो तुम कहां लिये जा रहे हो ? तुमसे किसने कहा था अर्जुन रोड चलने को ? उतारो मुझे’’, मैं कहते कहते चिल्ला पड़ी।
‘‘लाइए, पैसे लाइए इतनी दूर के।’’
‘‘कैसे पैसे ? दूर कहां ? अभी ही तो बैठी हूं और अभी ही तो उतर गयी हीं’’, मैं झटपट उतरकर चल दी अटपटाती चाल में।
‘‘पागल लगती है यह लड़की !’’
मुझे इस वाक्य में क्रोध के बदले अपना बचाव नज़र आया। मैं चुप सामने दिखने वाली लंबी काली सड़क को तेज़ी से नापने लगी। एक बार जल्दी में पांव मुड़ गया और चप्पल की तनी टूट गयी। एक बार साड़ी पांव के नीचे आ गयी और गिरते-गिरते बची। पीछे से कार सर्र करती मुझे धूल में रौंदती हुई निकल गयी। स्कूटर वाला आगे से पीछे की ओर तथा फिर पीछे से आगे की ओर थोड़ी-थोड़ी देर बाद निकल जाता कहता हुआ, ‘‘चलो केवल एक रुपये में पहुँचा देता हूं।’’
अरे तो क्या इसने सचमुच ही मुझे पागल समझ लिया है ? एक लसूड़ा घर आ रहा है और कई लसूड़े राह चलते मिल जाते हैं।
मैंने बचाव के लिए भीड़ को इधर-उधर ढूंढा तो दादा ने हांक लगायी, अरी ओर मूर्खा ! तेरे मन की ये फितूरबाजी और सूनी सड़कों पर भटकती करतूतें यदि तेरे मां पा को पता चलें तो वे क्या सोचें ? मत भूल कि एक लड़की है और लड़की को हर कदम पर सावधान रहना पड़ता है।’’
चलो गोली मारो उस साक्षात्कार को, कौन सी वह नौकरी मुझे ही मिलने वाली है ? खुद तो बहुत चल ली, अब क्यों न दूसरों को चलते हुए देखा जाये ? इस जीवन में कुछ और न बन पायें, पर इतने भी गये गुज़रे तो नहीं कि दर्शक भी न बन पायें। यदि दुनिया में दर्शक न होते तो सारे सांस्कृतिक क्रिया-कलाप ठप हो चुके होते। दर्शक जाति की अपनी ही महिमा है जो करोड़ों की फिल्म को एक नज़र में हिट और पिट करती है।
आ हा ! फिल्म का नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। अपने फिल्मी उत्साह की चपेट में जो भी मेरे आसपास होता है, उसे मैं अपने साथ बहा ले जाती हूं। लोगों को उनके ज़रूरी काम बिसरा देती हूं और इनकारी के सारे दरवाज़े- खिड़कियां बंद कर देती हूं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i