|
नारी विमर्श >> एक थी रामरती एक थी रामरतीशिवानी
|
426 पाठक हैं |
|||||||
शिवानी के मन को छूते हुए संस्मरण
एक थी रामरती
'एक था राजा' कहें या ‘घनदर्प-कंदर्प-सौन्दर्य हृद्यनिरवद्य भूपो वभूव,' अर्थ
एक ही होगा, किन्तु जो सहजता 'एक था राजा' में है, वह दूसरी छंदोमयी भाषा के
शब्दजाल में नहीं, इसी से लिख रही हूँ, 'एक थी रामरती' --यद्यपि उस नाम के साथ
भूतकाल का प्रयोग करने में मुझे वैसा ही कष्ट हो रहा है जैसा किसी प्रियजन को
तिलांजलि देने में, उसके नाम के आगे ‘प्रेत' शब्द जोड़ने में होता है।
गुरुवर द्विवेदीजी ने अपने एक भाषण में कभी बड़ी महत्त्वपूर्ण बात कही थी, “आपके इर्द-गिर्द जो जानता है, वह बहुत बड़ी चीज है। उसकी परम्परा महान् है, उसी को आप अपने अध्ययन का प्रधान विषय बनायें। आपको इसी जनता के निकट सम्पर्क में रहकर कार्य करना है। आस-पास की जनता की भाषा, विचार, जाति-पाँति, रहन-सहन, धर्म-कर्म सबकुछ के विषय में ज्ञानसंग्रह करने का प्रयत्न कीजिए, पुस्तकालय और संग्रहालय को अपने कार्य का अत्यन्त आवश्यक अंग तो समझिए ही, किन्तु जनता को प्रबुद्ध बनाना आपका काम है। उसे इस योग्य बनाएँ कि वह अपने अतीत को समझ सके, वर्तमान को देख सके और भविष्य को बना सके। अर्थात् जनता से ही सीखें, उसी को सिखाएँ।”
इसमें कोई सन्देह नहीं कि असंख्य वाचनालय हमें मानवता का वह पाठ पढ़ाने में सक्षम नहीं हो सकते, जो पाठ हमें हमारे पास की जनता अनायास ही पढ़ा जाती है। अपने दीर्घ जीवन के अनेकानेक रहस्यमय कोष्ठ-प्रकोष्ठों की परिक्रमाएँ मुझे कभी ऐसी ही अनूठी अभिज्ञताएँ थमा गई हैं। जीवन में अनेक उदार कृती गुरुजनों की शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किन्तु कभी-कभी लगता है, जीवन के जो अनुभूत मृत्युंजयी टोटके अपढ़ या सामान्य शिक्षित जनता ने थमाए, जीवन की दुरूह पगडंडियों को पराजित करने की क्षमता उन्हीं से प्राप्त की। आज, जब एक ऐसी ही अपढ़ सरल, विलक्षण सद्यःदिवंगता सेविका को. कतज्ञ करपट श्रद्धासमन अर्पित करने तत्पर होते हैं तो एक पल को वह आनन्दी हँसमुख चेहरा, कंठ वाष्प स्तम्भित कर देता है। दुबली-पतली देह, वजन कुल 29 किलो, जिसे यत्न से सींचने पर भी कभी वजन तौलने की मशीन की सुई मैं रंचमात्र भी आगे नहीं खिसका पाई किन्तु प्राणशक्ति उतनी ही वजनदार। कभी-कभी आश्चर्य होता था कि उस मुट्ठीभर देह में इतनी शक्ति आती कहाँ से है! उसके प्रेममय सहज हृदय की सरलता देखकर सहसा विश्वास नहीं होता था कि इस कुटिल युग में भी किसी का हृदय इतना निष्कपट, ऐसा निष्कलुष और निःस्वार्थ हो सकता है।
समझ में नहीं आता कहाँ से आरम्भ करूँ, पर इतना अवश्य समझ रही हूँ कि एकदम सतर, सीधी सरल रेखा खींचना कितना कठिन होता है। न वह उच्च कुल में जनमी, न शिक्षा ही प्राप्त की, न आभिजात्य, न अहंकार, इस स्मृतिचित्र को आँकने में न कल्पना का ही सहारा ले सकती हूँ, न छंदोमयी भाषा का। बाईस वर्ष पूर्व मैंने उसकी नियुक्ति की तो मेरे पति ने घोर आपत्ति की थी, “इतने काम करनेवाले तो हैं! फिर यह कई घरों में काम करती है, दस घरों का जूठन यहाँ फैलाएगी, हमारे यहाँ अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रह जाएगी।”
“वह ऐसी नहीं लगती,” मैंने दृढ़ स्वर में कहा। और उसी दिन से उसने हमारे गृह की सेविका का भार सँभाल लिया। वर्षों पश्चात्, जब मेरे पति मृत्युशय्या पर पड़े थे, तो उन्होंने कहा था, “तुमने इसे ठीक ही पहचाना था। यह हमेशा तुम्हारा सहारा बनेगी।” यद्यपि उस दिन पति का वह समर्थन मुझे मन-ही-मन विषण्ण कर गया था। उनके नैराश्यपूर्ण स्वर में अब मेरा सहारा न बने रहने का स्पष्ट संकेत था। उनकी मृत्यु के पश्चात् सचमुच ही उसने मेरी लड़खड़ाती गृहस्थी का संपूर्ण भार अपने दुर्बल कन्धों पर साध लिया। विछोह के प्रारम्भिक क्षणों में शायद विवेकशीलता एवं धैर्य के आयुध विधाता बड़ी हृदयहीनता से छीन लेता है। यह जानकर भी कि उस आघात को मुझे अकेले ही झेलना होगा, वह भी अडिग साहस से, मैं प्रतिपल हताश होकर धैर्यच्युत हुई जा रही थी। पति की ईमानदारी ने लक्ष्मी को बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था, न कोई संचित धनराशि थी, न किसी जीवन बीमे के तिनके का सहारा। लिखने की चेष्टा करती तो लेखनी अड़ियल-अबाध्य अश्व बनी हिनहिनाकर दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती। ‘नहिं विद्या नहिं बाहुबल नहिं खर्चन को दाम' वाली स्थिति मुझे किंकर्तव्यविमूढ़ बना रही थी। इसी से मैंने उससे कहा, “रामरती, अब तुम्हें नहीं रख पाऊँगी। तुम कोई और घर देख लो।" तब तक उसका पूरा परिवार मुझ पर ही निर्भर था। अचानक उसके पति की नौकरी चली गई थी। तीन-तीन बेटियाँ थीं, उसे तो अपना पेट पालना ही होगा। “ल्यो, अउर सुनो!" वह सींकिया देह को सतरकर खड़ी हो गई थी, "कहती हैं अउर घर देख लो! हम का तोहका अइसन घड़ी में छोड़ देई? हम का नमकहराम बिलार हैं दीदी, जो मालिक घरै दूध न मिली तो अंतै चली जाई?"
और वह नहीं गई, पर मेरे लाख कहने पर भी उसने तब तक वेतन नहीं लिया जब तब मुझे अपने पति का फंड, पेंशन-राशि नहीं मिली। मेरी मँझली पुत्री विदेश में थी, छोटी ससुराल में, छोटा पुत्र पढ़ रहा था। बड़ी पुत्री तीन महीने मेरे साथ रही, फिर उसे भी विदेश जाना पड़ा। जिस दिन वह गई, उसी रात को रामरती अपनी गुदड़ी-कंथरी सिर पर धरे, रात को सहसा मेरे कमरे में हँसती खड़ी हो गई, “महतारी, ल्यो, हम आइ गईन।” फिर मजाल थी जो अर्धरात्रि के किसी दुर्वह क्षण में उससे छिपाकर मैं एक सिसकी तो कंठ में घुटक लूँ! मेरा निःशब्द रुदन भी उसके चौकन्ने कानों तक पहुँच जाता। वह तत्काल उठकर कठोर प्रहरी-सी मेरे सिरहाने खड़ी हो जाती-“आँखिन का फोर डरियो का? देखो दीदी, तोहार रोये-धोये से अब साहेब लौटिहैं का?"
मुझे खिलाने-पिलाने में वह फिर स्नेहशील जननी बनी। मेरे एक-एक गस्से का हिसाब रखती-रोटी क्यों छोड़ दी?...दूध क्यों नहीं पिया?
उस आघात के पश्चात्, उसी ने मुझे काग़ज़-कलम थमा एक दिन जबरदस्ती लिखने बिठा दिया था, “थामो, लिख डारो तनी, जान्यो दीदी, जब हमार कड़ियल जवान मामा गवा रहा, हमार नानी रात-भर चकिया पीसत रही। हम उठिन की तनी नानी का हाथ बँटा दें, मार घुड़क दिहिन हमका, कहिन–'जा भाग जा, सो जा रतिया, हम का चकिया पीसत हैं? हम तो अपना दुख भुलाय रहिन!"
जीवन में पहली बार, अपने उस लेख को बिना दूसरी बार देखे मैंने ज्योंका-त्यों 'नवनीत' में भेज दिया था- 'बांधीश ने आर मायार डोरे', और जब सैकड़ों प्रशंसकों-पाठकों ने मुझे उस लेख के लिए बधाई के पत्र लिखे तो लगा, कैसी सवा लाख की सीख दी थी उस अनपढ़ नारी ने! लेखनी की चकिया पीस न केवल मेरे दुख की गठरी हलकी हुई मुझ जैसे अनेक विधुर आहत हृदयों का भी दुख हलका हुआ था।
कभी-कभी उसकी दार्शनिकता देख अवाक् रह जाती। एक दिन मैंने कहा, "रामरती, इस जीवन में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मुझे यह दंड क्यों दिया ?”
वह एक क्षण को निर्वाक् मूर्तिवत् बैठी रही, फिर बोली, “हम का इसी जिनगी का किया भोगत हैं दीदी? अरे पिछले जनम का हिसाब भी तो चुकता किए का परी! अब तुम जो दिन-रात तम्बाकू खात हो, तोहार बिटिया-बिटवा कहत हैं-रामरती, दीदी का तम्बाकू छुड़ाय दे, डिबिया छिपा दिया कर, कैंसर होत है-हम का छिपा सकिन हैं आज तलक? आपहु हमें दिन-रात डाँटत हैं कि बीड़ी मत पी, कलेजा मत फॅक, सो हम का छोड़ सकिन हैं? अरे, ई सब उई जनम केर अमल हैं, सब हमार करनी का अमल। रोग, जर-जमीन, केसमुकद्दमा, फाँसी, जेल, अमल सब सूद हैं सूद-उह जनम में लिए रहे, इहु जनम में चुकाय रहिन हैं। बड़ा जालिम सूदखोर महाजन है भगवान, जान्यो दीदी! जब तक एक-एक धेला न वसूली, छोड़ि है नाँही।"
मैं आश्चर्यचकित हो उसकी बातें सुन-सोच रही थी-न इसने कभी कोई धर्मग्रन्थ पढ़े, न मनीषियों की पंक्तियाँ ही सुनी, किन्तु फिर भी उनके मननचिंतन से उसकी सरल विचारधारा का यह कैसा अद्भुत साम्य था!
गुरुवर द्विवेदीजी ने अपने एक भाषण में कभी बड़ी महत्त्वपूर्ण बात कही थी, “आपके इर्द-गिर्द जो जानता है, वह बहुत बड़ी चीज है। उसकी परम्परा महान् है, उसी को आप अपने अध्ययन का प्रधान विषय बनायें। आपको इसी जनता के निकट सम्पर्क में रहकर कार्य करना है। आस-पास की जनता की भाषा, विचार, जाति-पाँति, रहन-सहन, धर्म-कर्म सबकुछ के विषय में ज्ञानसंग्रह करने का प्रयत्न कीजिए, पुस्तकालय और संग्रहालय को अपने कार्य का अत्यन्त आवश्यक अंग तो समझिए ही, किन्तु जनता को प्रबुद्ध बनाना आपका काम है। उसे इस योग्य बनाएँ कि वह अपने अतीत को समझ सके, वर्तमान को देख सके और भविष्य को बना सके। अर्थात् जनता से ही सीखें, उसी को सिखाएँ।”
इसमें कोई सन्देह नहीं कि असंख्य वाचनालय हमें मानवता का वह पाठ पढ़ाने में सक्षम नहीं हो सकते, जो पाठ हमें हमारे पास की जनता अनायास ही पढ़ा जाती है। अपने दीर्घ जीवन के अनेकानेक रहस्यमय कोष्ठ-प्रकोष्ठों की परिक्रमाएँ मुझे कभी ऐसी ही अनूठी अभिज्ञताएँ थमा गई हैं। जीवन में अनेक उदार कृती गुरुजनों की शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किन्तु कभी-कभी लगता है, जीवन के जो अनुभूत मृत्युंजयी टोटके अपढ़ या सामान्य शिक्षित जनता ने थमाए, जीवन की दुरूह पगडंडियों को पराजित करने की क्षमता उन्हीं से प्राप्त की। आज, जब एक ऐसी ही अपढ़ सरल, विलक्षण सद्यःदिवंगता सेविका को. कतज्ञ करपट श्रद्धासमन अर्पित करने तत्पर होते हैं तो एक पल को वह आनन्दी हँसमुख चेहरा, कंठ वाष्प स्तम्भित कर देता है। दुबली-पतली देह, वजन कुल 29 किलो, जिसे यत्न से सींचने पर भी कभी वजन तौलने की मशीन की सुई मैं रंचमात्र भी आगे नहीं खिसका पाई किन्तु प्राणशक्ति उतनी ही वजनदार। कभी-कभी आश्चर्य होता था कि उस मुट्ठीभर देह में इतनी शक्ति आती कहाँ से है! उसके प्रेममय सहज हृदय की सरलता देखकर सहसा विश्वास नहीं होता था कि इस कुटिल युग में भी किसी का हृदय इतना निष्कपट, ऐसा निष्कलुष और निःस्वार्थ हो सकता है।
समझ में नहीं आता कहाँ से आरम्भ करूँ, पर इतना अवश्य समझ रही हूँ कि एकदम सतर, सीधी सरल रेखा खींचना कितना कठिन होता है। न वह उच्च कुल में जनमी, न शिक्षा ही प्राप्त की, न आभिजात्य, न अहंकार, इस स्मृतिचित्र को आँकने में न कल्पना का ही सहारा ले सकती हूँ, न छंदोमयी भाषा का। बाईस वर्ष पूर्व मैंने उसकी नियुक्ति की तो मेरे पति ने घोर आपत्ति की थी, “इतने काम करनेवाले तो हैं! फिर यह कई घरों में काम करती है, दस घरों का जूठन यहाँ फैलाएगी, हमारे यहाँ अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रह जाएगी।”
“वह ऐसी नहीं लगती,” मैंने दृढ़ स्वर में कहा। और उसी दिन से उसने हमारे गृह की सेविका का भार सँभाल लिया। वर्षों पश्चात्, जब मेरे पति मृत्युशय्या पर पड़े थे, तो उन्होंने कहा था, “तुमने इसे ठीक ही पहचाना था। यह हमेशा तुम्हारा सहारा बनेगी।” यद्यपि उस दिन पति का वह समर्थन मुझे मन-ही-मन विषण्ण कर गया था। उनके नैराश्यपूर्ण स्वर में अब मेरा सहारा न बने रहने का स्पष्ट संकेत था। उनकी मृत्यु के पश्चात् सचमुच ही उसने मेरी लड़खड़ाती गृहस्थी का संपूर्ण भार अपने दुर्बल कन्धों पर साध लिया। विछोह के प्रारम्भिक क्षणों में शायद विवेकशीलता एवं धैर्य के आयुध विधाता बड़ी हृदयहीनता से छीन लेता है। यह जानकर भी कि उस आघात को मुझे अकेले ही झेलना होगा, वह भी अडिग साहस से, मैं प्रतिपल हताश होकर धैर्यच्युत हुई जा रही थी। पति की ईमानदारी ने लक्ष्मी को बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था, न कोई संचित धनराशि थी, न किसी जीवन बीमे के तिनके का सहारा। लिखने की चेष्टा करती तो लेखनी अड़ियल-अबाध्य अश्व बनी हिनहिनाकर दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती। ‘नहिं विद्या नहिं बाहुबल नहिं खर्चन को दाम' वाली स्थिति मुझे किंकर्तव्यविमूढ़ बना रही थी। इसी से मैंने उससे कहा, “रामरती, अब तुम्हें नहीं रख पाऊँगी। तुम कोई और घर देख लो।" तब तक उसका पूरा परिवार मुझ पर ही निर्भर था। अचानक उसके पति की नौकरी चली गई थी। तीन-तीन बेटियाँ थीं, उसे तो अपना पेट पालना ही होगा। “ल्यो, अउर सुनो!" वह सींकिया देह को सतरकर खड़ी हो गई थी, "कहती हैं अउर घर देख लो! हम का तोहका अइसन घड़ी में छोड़ देई? हम का नमकहराम बिलार हैं दीदी, जो मालिक घरै दूध न मिली तो अंतै चली जाई?"
और वह नहीं गई, पर मेरे लाख कहने पर भी उसने तब तक वेतन नहीं लिया जब तब मुझे अपने पति का फंड, पेंशन-राशि नहीं मिली। मेरी मँझली पुत्री विदेश में थी, छोटी ससुराल में, छोटा पुत्र पढ़ रहा था। बड़ी पुत्री तीन महीने मेरे साथ रही, फिर उसे भी विदेश जाना पड़ा। जिस दिन वह गई, उसी रात को रामरती अपनी गुदड़ी-कंथरी सिर पर धरे, रात को सहसा मेरे कमरे में हँसती खड़ी हो गई, “महतारी, ल्यो, हम आइ गईन।” फिर मजाल थी जो अर्धरात्रि के किसी दुर्वह क्षण में उससे छिपाकर मैं एक सिसकी तो कंठ में घुटक लूँ! मेरा निःशब्द रुदन भी उसके चौकन्ने कानों तक पहुँच जाता। वह तत्काल उठकर कठोर प्रहरी-सी मेरे सिरहाने खड़ी हो जाती-“आँखिन का फोर डरियो का? देखो दीदी, तोहार रोये-धोये से अब साहेब लौटिहैं का?"
मुझे खिलाने-पिलाने में वह फिर स्नेहशील जननी बनी। मेरे एक-एक गस्से का हिसाब रखती-रोटी क्यों छोड़ दी?...दूध क्यों नहीं पिया?
उस आघात के पश्चात्, उसी ने मुझे काग़ज़-कलम थमा एक दिन जबरदस्ती लिखने बिठा दिया था, “थामो, लिख डारो तनी, जान्यो दीदी, जब हमार कड़ियल जवान मामा गवा रहा, हमार नानी रात-भर चकिया पीसत रही। हम उठिन की तनी नानी का हाथ बँटा दें, मार घुड़क दिहिन हमका, कहिन–'जा भाग जा, सो जा रतिया, हम का चकिया पीसत हैं? हम तो अपना दुख भुलाय रहिन!"
जीवन में पहली बार, अपने उस लेख को बिना दूसरी बार देखे मैंने ज्योंका-त्यों 'नवनीत' में भेज दिया था- 'बांधीश ने आर मायार डोरे', और जब सैकड़ों प्रशंसकों-पाठकों ने मुझे उस लेख के लिए बधाई के पत्र लिखे तो लगा, कैसी सवा लाख की सीख दी थी उस अनपढ़ नारी ने! लेखनी की चकिया पीस न केवल मेरे दुख की गठरी हलकी हुई मुझ जैसे अनेक विधुर आहत हृदयों का भी दुख हलका हुआ था।
कभी-कभी उसकी दार्शनिकता देख अवाक् रह जाती। एक दिन मैंने कहा, "रामरती, इस जीवन में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मुझे यह दंड क्यों दिया ?”
वह एक क्षण को निर्वाक् मूर्तिवत् बैठी रही, फिर बोली, “हम का इसी जिनगी का किया भोगत हैं दीदी? अरे पिछले जनम का हिसाब भी तो चुकता किए का परी! अब तुम जो दिन-रात तम्बाकू खात हो, तोहार बिटिया-बिटवा कहत हैं-रामरती, दीदी का तम्बाकू छुड़ाय दे, डिबिया छिपा दिया कर, कैंसर होत है-हम का छिपा सकिन हैं आज तलक? आपहु हमें दिन-रात डाँटत हैं कि बीड़ी मत पी, कलेजा मत फॅक, सो हम का छोड़ सकिन हैं? अरे, ई सब उई जनम केर अमल हैं, सब हमार करनी का अमल। रोग, जर-जमीन, केसमुकद्दमा, फाँसी, जेल, अमल सब सूद हैं सूद-उह जनम में लिए रहे, इहु जनम में चुकाय रहिन हैं। बड़ा जालिम सूदखोर महाजन है भगवान, जान्यो दीदी! जब तक एक-एक धेला न वसूली, छोड़ि है नाँही।"
मैं आश्चर्यचकित हो उसकी बातें सुन-सोच रही थी-न इसने कभी कोई धर्मग्रन्थ पढ़े, न मनीषियों की पंक्तियाँ ही सुनी, किन्तु फिर भी उनके मननचिंतन से उसकी सरल विचारधारा का यह कैसा अद्भुत साम्य था!
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i 






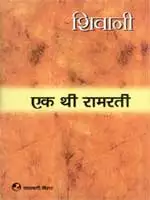


_s.jpg)
