|
नारी विमर्श >> एक थी रामरती एक थी रामरतीशिवानी
|
426 पाठक हैं |
|||||||
शिवानी के मन को छूते हुए संस्मरण
शिवानी हिन्दी की एकमात्र लेखिका हैं, जिन्होंने विपुल लेखन
किया और लोकप्रियता में भी सबसे आगे गई।
शिवानी की रचनाओं का अद्भुत संकलन है एक थी रामरती। एक जीवन्त पात्र
रामरती को लेकर लिखा गया यह मार्मिक कथात्मक संस्मरण उन्हें बेहद प्रिय था,
जो पाठकों को भी अभिभूत करेगा। पुस्तक में एक अन्तरंग बातचीत भी हैं, जो
शिवानी के जीवन से आपको परिचित कराएगी।
व्यक्ति-चित्र,स्मृति में केन्द्रित चिन्तन और विचार-प्रवाह की महिमा से
मंडित यह पुस्तक कथा-रस में डूबी हुई है और पाठक को एक जीवन्त संसार के
रू-ब-रू ला खड़ा करती है।
(अंतरंग बातचीत)
(लोकप्रिय कथा शिल्पी :शिवानी)
प्रश्न : शिवानी जी, आपके बहुत कम पाठक आपका असली नाम जानते
हैं। आपका असली नाम क्या है और आपने साहित्यिक उपनाम कब और क्यों रखा ? क्या
उपनाम के पीछे कोई विशेष कारण रहा ?
उत्तर : मेरा नाम वैसे गौरा है मैंने धर्मयुग में 1951 में एक छोटी कहानी—‘मैं मुर्गा हूँ’—लिखी थी। उसमें शिवानी नाम दिया था। मुझे शान्ति निकेतन (पश्चिमी बंगाल) में गुरुदेव (रवीन्द्रनाथ ठाकुर) के सान्निध्य में नौ वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। बांग्ला में ‘गौरा’ नहीं होता। गुरुदेव भी मुझे ‘गोरा’ कहकर पुकारते थे। वहां सब मुझे टोकते थे कि ‘गोरा’ नाम तो लड़कों का होता है। बांग्ला की एक पत्रिका थी—‘सोनार बांग्ला’। उसमें भी मैंने ‘मारीचिका’ नामक एक कहानी लिखी थी। लेकिन नाम उसमें भी गौरा ही छपा था। गौरा नाम छोड़कर साहित्यिक नाम शिवानी रखने के पीछे और कोई विशेष कारण नहीं है।
प्रश्न : साहित्य में आप किस-किससे प्रभावित रही हैं ? और किसने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया ? यानी आपके लेखन पर किसकी सर्वाधिक छाप पड़ी है ?
उत्तर : मैंने बांग्ला माध्यम से पढ़ा है। बांग्ला के प्रायः सभी स्वनामधन्य लेखकों को मैंने पढ़ा है। अतएव उनका प्रभाव मेरी भाषा पर पड़ा है। भाषा की दृष्टि से बंकिम ने मुझे विशेष प्रभावित किया। फिर मेरा जन्म गुजरात में हुआ था। मेरी मां गुजरात की विदुषी थी। गुजराती साहित्य भी मैंने पढ़ा। उसका प्रभाव भी मेरे लेखन पर पड़ा। गुजरात में हमारा घर साहित्यिक गतिविधियों का केन्द्र था। मेरे पिताजी अंग्रेजी के विद्वान् थे। ‘एशिया’ नामक अंग्रेजी मैगजीन में उनके लेख छपते थे। घर-परिवार में पठन-पाठन का वातावरण था। सच बात तो यह है कि बचपन से पढ़ने-लिखने के अलावा हमारा ध्यान किसी और बात की तरफ गया ही नहीं। बदलते हुए फ़ैशन ने भी हमें आकृष्ट नहीं किया।
प्रश्न : साहित्यकार भोगे हुए सत्य के कंकाल पर कल्पना का हाड़-मांस चढ़ाकर उसमें शब्दों और शैली की सांस फूंककर पाठकों के समक्ष रोबोट नहीं, बल्कि एक जीवंत चरित्र पेश करने की कोशिश करता है। आपका इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?
उत्तर : बिना यथार्थ के कोई भी रचना प्रभाव उत्पन्न करनेवाली नहीं हो सकती। वह युग चला गया जब केवल काल्पनिक सुख का दृश्य दिखाकर आकृष्ट किया जाता रहा। आज यथार्थ इतना कठिन और संघर्षपूर्ण है कि यदि उसे कल्पना चित्रित करने की कोशिश करेंगे तो पाठक स्वीकार नहीं करेगा। फिर जरूरी नहीं है कि आप हर यथार्थ को भोगें ही। सुनकर और देखकर भी आप उसे ज्यों-का-त्यों चित्रित कर सकते हैं।
प्रश्न : आपने जो चरित्र लिए हैं, क्या वे वास्तविक जीवन से हैं ? अपनी कृतियों में तांत्रिकों, योगियों और यहाँ तक की धूर्त साधुओं का यत्र-तत्र यथेष्ट उल्लेख किया है। क्या आपका ऐसे चरित्रों से वास्तविक जीवन में साबिका पड़ा है ?
उत्तर : जी हां, मैंने अपने अधिसंख्य चरित्र वास्तविक जीवन से ही लिए हैं। मैंने सुने सुनाए चरित्रों पर कभी कलम नहीं चलाई। मैंने अपने परिवार में जहां एक ओर कठोर सनातनी पक्ष देखा है वहां दूसरी ओर अति आधुनिक रंग-ढंग भी देखे। मुझे देश-विदेश घूमने-फिरने का अवसर भी मिला। मेरे पितामह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में धर्मोपदेशक थे। कट्टर सनातनी थे। खाना पकाने के लिए लकड़ियों तक को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करते थे महामना पंडित मदनमोहन मालवीय उनका बड़ा सम्मान करते थे। मालवीय जी अपने हाथ के कते हुए सूत से बने हुए वस्त्र उन्हें भेंटस्वरूप दिया करते थे। दादाजी अल्मोड़ा और बनारस में रहते थे। सो मेरा बचपन उनके साथ उक्त स्थानों पर बीता। पिताजी अधुनिक विचारों के पोषक थे।
दादा जी संस्कृत के प्रकांड पंडित तो थे ही साथ ही तंत्र साधना पर भी उनका असाधारण अधिकार था। मुझे स्मरण है कि बनारस में जब स्वामी विवेदानन्द पधारे थे तब उनके स्वागत उपलक्ष्य में जो संस्कृत में लिखा मानपत्र भेंट किया गया था, वह मेरे दादा जी ने ही लिखा था।
वृद्धावस्था में दादा जी की आंखें चली गई थीं। तब मैं ही उन्हें पढ़कर सुनाया करती थी। सो साधु-संतों में मेरी बचपन से ही रुचि रही। मैं मानती हूं कि विश्व में कोई ऐसी दैवी शक्ति है जिसकी विज्ञान कभी व्याख्या नहीं कर सकता। दादा जी की मित्र मंडली में नीलकंठ बाबा और गणेशपुरी के सुप्रसिद्ध संत नित्यानंद जैसे अनेक तपोनिष्ठ सिद्ध थे। और नित्यानंद जी तो ऐसे संत थे जिन्होंने कभी भी हमारी घर की देहरी नहीं लांघी-घर के अंदर नहीं आए। इनके अतिरिक्त आनन्दमयी मां को भी मैंने अपने परिवार में निकट से देखा है। वे मेरे चाचा जी देवीदत्त पांडे, जो जीवनपर्यन्त अविवाहित रहे, को अपना पुत्र मानती थीं। ऐसे संतों को मैंने निकट से देखा और सुना है। ‘भैरवी’ में मैंने अघोरी साधु का सच्चा वर्णन किया है।
प्रश्न : आप अपनी सर्वोत्तम कृति या रचना किसे मानती हैं ? क्या लेखक और पाठक की इस संबंध में अलग-अलग धारणाएं हो सकती हैं ? आपकी क्या राय है ?
उत्तर : मेरे लिए यह कहना कठिन है कि मेरी कौन-सी रचना सर्वोत्तम है। जिस तरह से किसी मां के लिए उसके बच्चे समान रूप से प्रिय होते हैं उसी प्रकार मुझे अपनी सभी कृतियां एक-सी प्रिय हैं। वैसे पाठकों ने अभी तक जिस कृति को सर्वाधिक सराहा है, वह है—‘कृष्णकली’। फिर भी यदि आप प्रिय रचना कहकर मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं यात्रावृत्तांत ‘चरैवेति’ का नाम लूंगी। इसमें भारत से मास्को तक की यात्रा का विवरण है। मेरी प्रिय रचना यही है। क्योंकि मैंने इसे अत्यधिक परिश्रम और ईमानदारी से लिखा है। हालाँकि आलोचकों ने इस कृति को न जाने क्या सोचकर उल्लेख योग्य नहीं समझा और न ही समीक्षकों ने कहीं इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा है।
प्रश्न : आपने किस अवस्था से लिखना शुरू किया ? पहली रचना कब और कहां छपी थी ? तब कैसा लगा था ? और अब ढेर सारा छपने पर कैसा लग रहा है ?
उत्तर : मेरी पहली रचना तब छपी जब मैं मात्र बारह वर्ष की थी, अल्मोड़ा से ‘नटखट’ नामक एक पत्रिका में पहली रचना छपी थी। उसके पश्चात् में शान्ति निकेतन चली गई। वहां हस्तलिखित पत्रिका निकलती थी। उसमें मेरी रचनाएं नियमित रूप से छपती थीं। तब रचना छपने पर बहुत आनन्द आया। अब कुछ ऐसा नहीं लगता कि उसे अभिव्यक्त करूं। फिर भी, आज भी जब कोई रचना छपती है तो खुशी तो होती है। सच कहूं तो लिखना मेरे लिए नशा है। जैसे किसी शराबी की लत होती है, बिना पिए वह रह नहीं सकता, ठीक वही दशा मेरी है। मैं बिना लिखे रह नहीं सकती। फिर भले ही एक पंक्ति ही क्यों न लिखूं, लेकिन प्रतिदिन लिखती अवश्य हूं।
प्रश्न : आपके साहित्य सृजन का क्या उद्देश्य रहा है—लोक कल्याण, आत्मसुख जिसके अन्तर्गत धन की प्राप्ति का लक्ष्य भी शामिल है या कुछ और ?
उत्तर : मैंने धन-संग्रह को कभी जीवन में प्रश्रय नहीं दिया। वैसे पैसा किसे अच्छा नहीं लगता, किन्तु केवल पैसे के लिए ही मैंने साहित्य सृजन नहीं किया। मैं पेशेवर लेखिका हूं। अपनी रचना का मूल्य चाहती हूं। फिर एक बात साफ है कि कोई भी लेखक-लेखिका स्वांतः सुखाय ही नहीं लिखता। जो रचना जनसाधारण को ऊंचा नहीं उठाती, उसे सोचने-समझने के लिए विवश नहीं करती, मैं उसे साहित्य नहीं मानती। जो साहित्यकार समाज में व्याप्त विकृतियों पर प्रहार नहीं करता उसका साहित्य-सृजन किस काम का ? अस्तु, मैंने दोनों ही दृष्टियों से लिखा है। लेकिन एक बात जोर देकर कहना चाहूंगी कि मैंने साहित्य सृजन किया है, शब्दों का व्यापार नहीं किया और लेखन के बदले जो कुछ सहजता से मिल गया, उसे स्वीकर कर लिया।
प्रश्न : आपके पाठकों और खास-तौर से समालोचकों का कहना है कि आपकी भाषा क्लिष्ट, संस्कृतनिष्ठ और सामासिक होती है। वाक्यविन्यास इतने बड़े और जटिल होते हैं कि अर्द्धविरामों की भरमार के कारण अर्थ समझने के लिए मस्तिष्क पर काफी जोर डालना पड़ता है। इससे साहित्य रसानुभूति के आनन्द में व्यवधान पड़ता है। क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं ?
उत्तर : आलोचकों को मैं कोई महत्व नहीं देती। उन्होंने मेरे साथ कभी न्याय नहीं किया। मैंने बचपन में अमरकोश पढ़ा। संस्कृत पढ़ी। घर में मां संस्कृत की विदुषी थीं और दादा जी संस्कृत के प्रकांड पंडित। दोनों का मुझ पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। मैं शब्दकोश खोलकर नहीं लिखती। जो भाषा बोलती हूं, वैसा ही लिखती हूं। उसे बदल नहीं सकती। फिर जब कठिन शब्द भावों को सम्प्रेषित करने में सक्षम होते हैं और रचना का रसास्वादन करने में आनन्द की अनुभूति होती है, तब मैं नहीं समझती कि जान-बूझकर सरल और अपेक्षाकृत कम प्रभावोत्पादक शब्दों का रखना कोई बुद्धिमत्ता है।
प्रश्न : आपने अब तक काफी साहित्य रचा है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं ?
उत्तर : जहां तक संतुष्ट होने का संबंध है, मैं समझती हूं कि किसी को भी अपने लेखन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि ऐसे लक्ष्य को सामने रखकर कुछ ऐसा लिखूं कि जिस परिवेश को पाठक ने स्वयं भोगा है, उसे जीवंत कर दूं। मुझे तब बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई पाठक मुझे लिख भेजता है कि आपने अमुक-अमुक चरित्र का वास्तविक वर्णन किया है अथवा फलां-फलां चरित्र, लगता है, हमारे ही बीच है। लेकिन साथ ही मैं यह मानती हूं कि लोकप्रिय होना न इतना आसान है और न ही उसे बनाए रखना आसान है। मैं गत पचास वर्षों से बराबर लिखती आ रही हूं। पाठक मेरे लेखन को खूब सराह रहे हैं। इसलिए निराशा का तो कोई कारण ही नहीं है। फिर मैं आलोचकों को कोई महत्व नहीं देती। मेरे असली आलोचक तो मेरे पाठक हैं, जिनसे मुझे प्रशंसा और स्नेह भरपूर मात्रा में मिलता रहा है। शायद यही कारण है कि मैं अब तक बराबर लिखती आई हूं।
प्रश्न : क्या कभी आपको फिल्मों के लिए काम करने का आफर आया है ? आप उस दुनिया की तरफ क्यों नहीं गईं, जबकि वहां पैसा भी काफी अच्छा है ?
उत्तर : बहुत आया। मेरी एक कहानी का तो फिल्म वालों ने सर्वनाश ही कर दिया। विनोद तिवारी ने बनाई थी फिल्म ‘करिये छिमा’ पर। इसके अतिरिक्त ‘सुरंगमा’, ‘रति विलाप’, ‘मेरा बेटा’, ‘तीसरा बेटा’—पर भी सीरियल बन रहे हैं। इसके बाद मैंने फिल्मों के लिए रचना देना बंद कर दिया और भविष्य में भी फिल्मों और दूरदर्शन के सीरियलों के लिए कहानी देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जो चीज को ही नष्ट कर दे, उस पैसे का क्या करना ?
प्रश्न : आपकी राय में साहित्यकार का समाज और अपने पाठकवर्ग के प्रति क्या दायित्व है ? आपने कैसे इस दायित्व का निर्वाह किया है ?
उत्तर : मैंने साहित्यकार के रूप में अपना दायित्व कहां तक निभाया, यह तो कहना कठिन है, लेकिन जहां तक साहित्यकार का सम्बन्ध है, मैं उसे राजनीतिज्ञ से अधिक महत्व देती हूं। क्योंकि कलम में वह ताकत है जो राजदंड में भी नहीं है।
प्रश्न : आप लेखन कार्य कब करती हैं ? लिखने के लिए विशेष मूड बनाती हैं या किसी भी स्थिति में लिख सकती हैं ?
उत्तर : ईमानदारी से कहूं तो मैं किसी भी स्थिति और परिस्थिति में लिख सकती हूं। सब्जी छौंकते हुए भी लिख सकती हूं और चाय की चुस्की लेते हुए भी लिख सकती हूं। रात को ज्यादा लिखती हूं, क्योंकि तब वातावरण शांत होता है। लेकिन यदि काम का भार पड़ जाता है तो दिन-रात किसी भी वक्त लिख लेती हूं। ‘कालिंदी’ को मैंने रात में भी लिखा और दिन भी में भी। एकांत में लिखना मुझे अच्छा लगता है।
प्रश्न : एक कहानी को आप कितनी बैठकों या सीटिंग में पूरा कर लेती हैं और लगातार कितनी देर तक लिखती हैं ?
उत्तर : पहले मैं मन में एक खाका बनाती हूं। फिर उसे कागज पर उतारती हूं। खाका बनाकर रफ लिखती हूं। हमेशा हाथ से लिखती हूं। यहां तक कि अंतिम आलेख तक भी हाथ से ही लिखकर छपने भेजती हूं। एक कहानी लिखने में मुझे पन्द्रह-बीस दिन लग जाते हैं। कम-से-कम दस-पन्द्रह दिन तो लगते ही हैं। लिखास लगती है तो लिखती हूं। मैंने दस-बारह सदस्यों के परिवार में भी लिखा है और जब बच्चे छोटे थे तब भी खूब लिखा। मेरे जीवन में कोई नाटकीय मोड़ नहीं है। मैं कभी बिस्तर पर बैठकर लिखती हूं तो कभी आंगन में चारपाई पर लिख लेती हूं तो कभी सोफे पर बैठकर ही लिख लेती हूं।
प्रश्न : हिन्दी का लेखन हमारे यहां अपेक्षाकृत अर्थाभाव का शिकार होता है। केवल लेखन के बल पर समाज में सम्मानजनक ढंग से जीवन यापन करना कल्पनातीत है। यदि आप शुरू से केवल लेखन से जीविका अर्जित करतीं तो क्या अपने वर्तमान स्तर को बनाए रख सकती थीं ?
उत्तर : मैं अपने लेखन के बल पर ही जीवित हूं। और एकदम स्वावलम्बी हूं। मैं मानती हूं कोई भी लेखक अपने लेखन के बल पर ही जीविका चलाकर सम्मानजनक ढंग से समाज में जीवनयापन कर सकता है, बशर्ते उसकी कलम में दम हो। कलम कमजोर है तो आमदनी भी कमजोर होगी।
प्रश्न : आमतौर से लेखन और परिवार दो विरोधाभासी चीजें मानी जाती रही हैं। आपके लेखन में परिवार आडे़ आया या उससे लेखन में मदद मिलती रही ?
उत्तर : मेरे लेखन में परिवार एक क्षण के लिए कभी भी आड़े नहीं आया। जब तक मेरे पति जीवित रहे, उन्होंने मुझे लेखन के लिए बराबर प्रोत्साहित किया। उनको मेरे लेखन पर गर्व था। मैं तब कोई भी रचना किसी भी पत्र-पत्रिका अथवा प्रेस में उनके पढ़े बिना नहीं भेजती थी। जब कभी मेरी किसी रचना में कोई व्यक्तित्व अथवा चरित्र उजागर होता है तो कहते-ऐसा न करो। वे मेरे एकमात्र सच्चे आलोचक थे। उनकी हिन्दी भी बहुत अच्छी थी। कभी मैं अपनी रचना उन्हें पढ़कर सुना दिया करती थी और कभी वे स्वयं पढ़कर आवश्यक सुझाव दे दिया करते थे।
प्रश्न : आपकी कौन-सी कृति सर्वाधिक चर्चित रही और सबसे अधिक आमदनी किस रचना से आपको हुई ?
उत्तर : ‘कृष्णकली’। अब तक उसके दस से अधिक संस्करण हो चुके हैं। यह पुस्तक देश के अनेक विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में लगी हुई है। जहाँ तक आमदनी का सवाल है, कोई पैसा दे देता है कोई पूछता भी नहीं। इस हालत में ठीक-ठीक बता पाना मुश्किल है कि किस रचना से कितनी आमदनी हुई। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि पाठकों से मुझे जो स्नेह मिला वह पैसे की तुलना में कहीं अधिक रहा है। रचना छपने पर पाठकों के ढेरों पत्र तो आते ही हैं, बल्कि कभी-कभी तो कोई पाठक स्नेह से अभिभूत होकर कोई वस्तु तक उपहार में भेज देता है। ऐसे ही एक बार मेरी किसी रचना को पढ़कर बिहार से एक प्रशंसक ने आम का एक पार्सल भेजा था। और मजे की बात यह कि उसने प्रेषक का नाम तक नहीं लिखा था। मैंने उसे धन्यवाद प्रेषित करने के लिए उसका पता-ठिकाना ढूंढ़ने की बहुत कोशिश की, किन्तु निर्रथक रही। लेकिन सबसे विचित्र अनुभव तो मुझे अपने स्नेही पाठकों का उस दिन हुआ था जब एक व्यक्ति, जो बेहद मामूली से कपड़े पहने था, शुद्ध घी का एक कनस्तर लेकर हमारे दरवाजे पर आया और पूछने पर जब मैंने बताया कि मैं ही शिवानी हूं, तो बोला, ‘‘मैं आपके लिए अपने घर से शुद्ध घी लाया हूं। आप बहुत अच्छा लिखती हैं।’’
घुटनों तक मैली-सी धोती और वैसी ही कमीज में निपट देहाती दिखने वाले उस पाठक को मैंने बहुत समझाया-बुझाया कि घी वापस ले जाओ लेकिन वह एक न माना और जब वह दरवाजे से बिना घी दिए टस-से-मस नहीं हुआ तो उसकी श्रद्धा का सम्मान करने के उद्देश्य से मैंने भरे हुए कनस्तर से पूजा के पात्र में थोड़ा-सा घी लेकर किसी तरह से उसे निराश न करते हुए विदा किया।
प्रश्न : देखने-सुनने में आता है कि लेखक की किसी एक रचना पर पाठक प्रतिक्रियास्वरूप उसे सूचित करता है कि आपने तो हू-ब-हू मेरा चरित्र उतार दिया है या अमुक चरित्र में मैं हूं या फलां चरित्र मेरा सगा-संबंधी या परिचित है। इसके अतिरिक्त इसके विपरीत भी झेलना पड़ता है, जब कभी कोई सिरफिरा रचना पढ़ते ही लड़ने-मरने को तैयार हो जाता है। अदालत का दरवाजा खटखटाने की धमकी दे देता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी घटा है ?
उत्तर : वैसे तो पाठक अकसर रचना पढ़कर पत्र भेजते रहते हैं कि आपने अमुक-अमुक व्यक्ति का चरित्र हू-ब-हू उतारा है। ऐसा इसलिए होता है कि मेरे पात्र वास्तविक घटनाओं से ही होते हैं। लेकिन एक बार एक कहानी छपने पर सचमुच मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। 1970 में ‘धर्मयुग’ में मेरी ‘हंसा जाई अकेला’ नाम की कहानी छपी। यह कहानी नाथद्वारा (राजस्थान) के एक महंत पर आधारित थी। कहानी छपते ही उनके चेलों ने हायतोबा मचा दी। मुकदमा करने तक की धमकी देने लगे। ‘धर्मयुग’ के तत्कालीन संपादक डॉ. धर्मवीर भारती को भी उन्होंने धमकी-भरे पत्र लिखे। भारती जी ने परेशान होकर मुझे लिखा। लेकिन मेरे पास प्रमाण था। मैंने उस सम्बन्ध में एक चित्र लाकर भारती जी को भेज दिया। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। स्पष्ट था कि भारती जी ने प्रमाणस्वरूप वह चित्र महंत के चेलों को दिखाया होगा, जिससे उनकी बोलती बंद हो गई होगी।
प्रश्न : क्या आप एक समय एक ही रचना पर कार्य करती हैं या एकाधिक विषयों पर काम करती रहती हैं ?
उत्तर : मैं जब एक चीज पर लिखना शुरू करती हूं तो उसे समाप्त करने के पश्चात् ही दूसरी चीज लिखना शुरू करती हूं। फिर एक चीज समाप्त करने के बाद कुछ दिन तक नहीं लिखती। उन दिनों लिखती हूं, लेकिन कहानी उपन्यास नहीं, बल्कि निबंध अथवा लेख-आलेख आदि लिखती हूं। मैं समझती हूं कि एक समय में एक से अधिक रचनाओं पर काम करने से ध्यान बंट जाता है। और रचना में वह खूबसूरती नहीं आ पाती जो कि आनी चाहिए।
प्रश्न : अक्सर व्यक्ति किसी घटना विशेष के कारण लेखक, कवि या साहित्यसर्जक बन जाते हैं। आपके लेखिका बनने के पीछे क्या कारण रहा है ?
उत्तर : जैसा कि मैं पहले कहती आई हूं कि हमारे परिवार का वातावरण मेरे लेखिका बनने के सर्वथा उपयुक्त था। फिर मैं नौ वर्ष शांति निकेतन में गुरुदेव के संरक्षण में रही इसका भी मुझ पर प्रभाव पड़ा। लिखने के प्रति मेरा रुझान बचपन से ही था। यों कह सकते हैं कि मेरे अंदर लेखिका बनने का बीज मौजूद था, और उपयुक्त वातावरण मिलने पर मैं लेखिका बन गई। मैं नहीं मानती कि कोई घटना से प्रभावित होकर लेखक बन सकता है। उदाहरण के लिए किसी प्रियजन की मृत्यु से दुःखी होकर कोई संन्यासी तो बन सकता है, किन्तु लेखक नहीं बन सकता।
उत्तर : मेरा नाम वैसे गौरा है मैंने धर्मयुग में 1951 में एक छोटी कहानी—‘मैं मुर्गा हूँ’—लिखी थी। उसमें शिवानी नाम दिया था। मुझे शान्ति निकेतन (पश्चिमी बंगाल) में गुरुदेव (रवीन्द्रनाथ ठाकुर) के सान्निध्य में नौ वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। बांग्ला में ‘गौरा’ नहीं होता। गुरुदेव भी मुझे ‘गोरा’ कहकर पुकारते थे। वहां सब मुझे टोकते थे कि ‘गोरा’ नाम तो लड़कों का होता है। बांग्ला की एक पत्रिका थी—‘सोनार बांग्ला’। उसमें भी मैंने ‘मारीचिका’ नामक एक कहानी लिखी थी। लेकिन नाम उसमें भी गौरा ही छपा था। गौरा नाम छोड़कर साहित्यिक नाम शिवानी रखने के पीछे और कोई विशेष कारण नहीं है।
प्रश्न : साहित्य में आप किस-किससे प्रभावित रही हैं ? और किसने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया ? यानी आपके लेखन पर किसकी सर्वाधिक छाप पड़ी है ?
उत्तर : मैंने बांग्ला माध्यम से पढ़ा है। बांग्ला के प्रायः सभी स्वनामधन्य लेखकों को मैंने पढ़ा है। अतएव उनका प्रभाव मेरी भाषा पर पड़ा है। भाषा की दृष्टि से बंकिम ने मुझे विशेष प्रभावित किया। फिर मेरा जन्म गुजरात में हुआ था। मेरी मां गुजरात की विदुषी थी। गुजराती साहित्य भी मैंने पढ़ा। उसका प्रभाव भी मेरे लेखन पर पड़ा। गुजरात में हमारा घर साहित्यिक गतिविधियों का केन्द्र था। मेरे पिताजी अंग्रेजी के विद्वान् थे। ‘एशिया’ नामक अंग्रेजी मैगजीन में उनके लेख छपते थे। घर-परिवार में पठन-पाठन का वातावरण था। सच बात तो यह है कि बचपन से पढ़ने-लिखने के अलावा हमारा ध्यान किसी और बात की तरफ गया ही नहीं। बदलते हुए फ़ैशन ने भी हमें आकृष्ट नहीं किया।
प्रश्न : साहित्यकार भोगे हुए सत्य के कंकाल पर कल्पना का हाड़-मांस चढ़ाकर उसमें शब्दों और शैली की सांस फूंककर पाठकों के समक्ष रोबोट नहीं, बल्कि एक जीवंत चरित्र पेश करने की कोशिश करता है। आपका इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?
उत्तर : बिना यथार्थ के कोई भी रचना प्रभाव उत्पन्न करनेवाली नहीं हो सकती। वह युग चला गया जब केवल काल्पनिक सुख का दृश्य दिखाकर आकृष्ट किया जाता रहा। आज यथार्थ इतना कठिन और संघर्षपूर्ण है कि यदि उसे कल्पना चित्रित करने की कोशिश करेंगे तो पाठक स्वीकार नहीं करेगा। फिर जरूरी नहीं है कि आप हर यथार्थ को भोगें ही। सुनकर और देखकर भी आप उसे ज्यों-का-त्यों चित्रित कर सकते हैं।
प्रश्न : आपने जो चरित्र लिए हैं, क्या वे वास्तविक जीवन से हैं ? अपनी कृतियों में तांत्रिकों, योगियों और यहाँ तक की धूर्त साधुओं का यत्र-तत्र यथेष्ट उल्लेख किया है। क्या आपका ऐसे चरित्रों से वास्तविक जीवन में साबिका पड़ा है ?
उत्तर : जी हां, मैंने अपने अधिसंख्य चरित्र वास्तविक जीवन से ही लिए हैं। मैंने सुने सुनाए चरित्रों पर कभी कलम नहीं चलाई। मैंने अपने परिवार में जहां एक ओर कठोर सनातनी पक्ष देखा है वहां दूसरी ओर अति आधुनिक रंग-ढंग भी देखे। मुझे देश-विदेश घूमने-फिरने का अवसर भी मिला। मेरे पितामह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में धर्मोपदेशक थे। कट्टर सनातनी थे। खाना पकाने के लिए लकड़ियों तक को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करते थे महामना पंडित मदनमोहन मालवीय उनका बड़ा सम्मान करते थे। मालवीय जी अपने हाथ के कते हुए सूत से बने हुए वस्त्र उन्हें भेंटस्वरूप दिया करते थे। दादाजी अल्मोड़ा और बनारस में रहते थे। सो मेरा बचपन उनके साथ उक्त स्थानों पर बीता। पिताजी अधुनिक विचारों के पोषक थे।
दादा जी संस्कृत के प्रकांड पंडित तो थे ही साथ ही तंत्र साधना पर भी उनका असाधारण अधिकार था। मुझे स्मरण है कि बनारस में जब स्वामी विवेदानन्द पधारे थे तब उनके स्वागत उपलक्ष्य में जो संस्कृत में लिखा मानपत्र भेंट किया गया था, वह मेरे दादा जी ने ही लिखा था।
वृद्धावस्था में दादा जी की आंखें चली गई थीं। तब मैं ही उन्हें पढ़कर सुनाया करती थी। सो साधु-संतों में मेरी बचपन से ही रुचि रही। मैं मानती हूं कि विश्व में कोई ऐसी दैवी शक्ति है जिसकी विज्ञान कभी व्याख्या नहीं कर सकता। दादा जी की मित्र मंडली में नीलकंठ बाबा और गणेशपुरी के सुप्रसिद्ध संत नित्यानंद जैसे अनेक तपोनिष्ठ सिद्ध थे। और नित्यानंद जी तो ऐसे संत थे जिन्होंने कभी भी हमारी घर की देहरी नहीं लांघी-घर के अंदर नहीं आए। इनके अतिरिक्त आनन्दमयी मां को भी मैंने अपने परिवार में निकट से देखा है। वे मेरे चाचा जी देवीदत्त पांडे, जो जीवनपर्यन्त अविवाहित रहे, को अपना पुत्र मानती थीं। ऐसे संतों को मैंने निकट से देखा और सुना है। ‘भैरवी’ में मैंने अघोरी साधु का सच्चा वर्णन किया है।
प्रश्न : आप अपनी सर्वोत्तम कृति या रचना किसे मानती हैं ? क्या लेखक और पाठक की इस संबंध में अलग-अलग धारणाएं हो सकती हैं ? आपकी क्या राय है ?
उत्तर : मेरे लिए यह कहना कठिन है कि मेरी कौन-सी रचना सर्वोत्तम है। जिस तरह से किसी मां के लिए उसके बच्चे समान रूप से प्रिय होते हैं उसी प्रकार मुझे अपनी सभी कृतियां एक-सी प्रिय हैं। वैसे पाठकों ने अभी तक जिस कृति को सर्वाधिक सराहा है, वह है—‘कृष्णकली’। फिर भी यदि आप प्रिय रचना कहकर मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं यात्रावृत्तांत ‘चरैवेति’ का नाम लूंगी। इसमें भारत से मास्को तक की यात्रा का विवरण है। मेरी प्रिय रचना यही है। क्योंकि मैंने इसे अत्यधिक परिश्रम और ईमानदारी से लिखा है। हालाँकि आलोचकों ने इस कृति को न जाने क्या सोचकर उल्लेख योग्य नहीं समझा और न ही समीक्षकों ने कहीं इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा है।
प्रश्न : आपने किस अवस्था से लिखना शुरू किया ? पहली रचना कब और कहां छपी थी ? तब कैसा लगा था ? और अब ढेर सारा छपने पर कैसा लग रहा है ?
उत्तर : मेरी पहली रचना तब छपी जब मैं मात्र बारह वर्ष की थी, अल्मोड़ा से ‘नटखट’ नामक एक पत्रिका में पहली रचना छपी थी। उसके पश्चात् में शान्ति निकेतन चली गई। वहां हस्तलिखित पत्रिका निकलती थी। उसमें मेरी रचनाएं नियमित रूप से छपती थीं। तब रचना छपने पर बहुत आनन्द आया। अब कुछ ऐसा नहीं लगता कि उसे अभिव्यक्त करूं। फिर भी, आज भी जब कोई रचना छपती है तो खुशी तो होती है। सच कहूं तो लिखना मेरे लिए नशा है। जैसे किसी शराबी की लत होती है, बिना पिए वह रह नहीं सकता, ठीक वही दशा मेरी है। मैं बिना लिखे रह नहीं सकती। फिर भले ही एक पंक्ति ही क्यों न लिखूं, लेकिन प्रतिदिन लिखती अवश्य हूं।
प्रश्न : आपके साहित्य सृजन का क्या उद्देश्य रहा है—लोक कल्याण, आत्मसुख जिसके अन्तर्गत धन की प्राप्ति का लक्ष्य भी शामिल है या कुछ और ?
उत्तर : मैंने धन-संग्रह को कभी जीवन में प्रश्रय नहीं दिया। वैसे पैसा किसे अच्छा नहीं लगता, किन्तु केवल पैसे के लिए ही मैंने साहित्य सृजन नहीं किया। मैं पेशेवर लेखिका हूं। अपनी रचना का मूल्य चाहती हूं। फिर एक बात साफ है कि कोई भी लेखक-लेखिका स्वांतः सुखाय ही नहीं लिखता। जो रचना जनसाधारण को ऊंचा नहीं उठाती, उसे सोचने-समझने के लिए विवश नहीं करती, मैं उसे साहित्य नहीं मानती। जो साहित्यकार समाज में व्याप्त विकृतियों पर प्रहार नहीं करता उसका साहित्य-सृजन किस काम का ? अस्तु, मैंने दोनों ही दृष्टियों से लिखा है। लेकिन एक बात जोर देकर कहना चाहूंगी कि मैंने साहित्य सृजन किया है, शब्दों का व्यापार नहीं किया और लेखन के बदले जो कुछ सहजता से मिल गया, उसे स्वीकर कर लिया।
प्रश्न : आपके पाठकों और खास-तौर से समालोचकों का कहना है कि आपकी भाषा क्लिष्ट, संस्कृतनिष्ठ और सामासिक होती है। वाक्यविन्यास इतने बड़े और जटिल होते हैं कि अर्द्धविरामों की भरमार के कारण अर्थ समझने के लिए मस्तिष्क पर काफी जोर डालना पड़ता है। इससे साहित्य रसानुभूति के आनन्द में व्यवधान पड़ता है। क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं ?
उत्तर : आलोचकों को मैं कोई महत्व नहीं देती। उन्होंने मेरे साथ कभी न्याय नहीं किया। मैंने बचपन में अमरकोश पढ़ा। संस्कृत पढ़ी। घर में मां संस्कृत की विदुषी थीं और दादा जी संस्कृत के प्रकांड पंडित। दोनों का मुझ पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। मैं शब्दकोश खोलकर नहीं लिखती। जो भाषा बोलती हूं, वैसा ही लिखती हूं। उसे बदल नहीं सकती। फिर जब कठिन शब्द भावों को सम्प्रेषित करने में सक्षम होते हैं और रचना का रसास्वादन करने में आनन्द की अनुभूति होती है, तब मैं नहीं समझती कि जान-बूझकर सरल और अपेक्षाकृत कम प्रभावोत्पादक शब्दों का रखना कोई बुद्धिमत्ता है।
प्रश्न : आपने अब तक काफी साहित्य रचा है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं ?
उत्तर : जहां तक संतुष्ट होने का संबंध है, मैं समझती हूं कि किसी को भी अपने लेखन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि ऐसे लक्ष्य को सामने रखकर कुछ ऐसा लिखूं कि जिस परिवेश को पाठक ने स्वयं भोगा है, उसे जीवंत कर दूं। मुझे तब बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई पाठक मुझे लिख भेजता है कि आपने अमुक-अमुक चरित्र का वास्तविक वर्णन किया है अथवा फलां-फलां चरित्र, लगता है, हमारे ही बीच है। लेकिन साथ ही मैं यह मानती हूं कि लोकप्रिय होना न इतना आसान है और न ही उसे बनाए रखना आसान है। मैं गत पचास वर्षों से बराबर लिखती आ रही हूं। पाठक मेरे लेखन को खूब सराह रहे हैं। इसलिए निराशा का तो कोई कारण ही नहीं है। फिर मैं आलोचकों को कोई महत्व नहीं देती। मेरे असली आलोचक तो मेरे पाठक हैं, जिनसे मुझे प्रशंसा और स्नेह भरपूर मात्रा में मिलता रहा है। शायद यही कारण है कि मैं अब तक बराबर लिखती आई हूं।
प्रश्न : क्या कभी आपको फिल्मों के लिए काम करने का आफर आया है ? आप उस दुनिया की तरफ क्यों नहीं गईं, जबकि वहां पैसा भी काफी अच्छा है ?
उत्तर : बहुत आया। मेरी एक कहानी का तो फिल्म वालों ने सर्वनाश ही कर दिया। विनोद तिवारी ने बनाई थी फिल्म ‘करिये छिमा’ पर। इसके अतिरिक्त ‘सुरंगमा’, ‘रति विलाप’, ‘मेरा बेटा’, ‘तीसरा बेटा’—पर भी सीरियल बन रहे हैं। इसके बाद मैंने फिल्मों के लिए रचना देना बंद कर दिया और भविष्य में भी फिल्मों और दूरदर्शन के सीरियलों के लिए कहानी देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जो चीज को ही नष्ट कर दे, उस पैसे का क्या करना ?
प्रश्न : आपकी राय में साहित्यकार का समाज और अपने पाठकवर्ग के प्रति क्या दायित्व है ? आपने कैसे इस दायित्व का निर्वाह किया है ?
उत्तर : मैंने साहित्यकार के रूप में अपना दायित्व कहां तक निभाया, यह तो कहना कठिन है, लेकिन जहां तक साहित्यकार का सम्बन्ध है, मैं उसे राजनीतिज्ञ से अधिक महत्व देती हूं। क्योंकि कलम में वह ताकत है जो राजदंड में भी नहीं है।
प्रश्न : आप लेखन कार्य कब करती हैं ? लिखने के लिए विशेष मूड बनाती हैं या किसी भी स्थिति में लिख सकती हैं ?
उत्तर : ईमानदारी से कहूं तो मैं किसी भी स्थिति और परिस्थिति में लिख सकती हूं। सब्जी छौंकते हुए भी लिख सकती हूं और चाय की चुस्की लेते हुए भी लिख सकती हूं। रात को ज्यादा लिखती हूं, क्योंकि तब वातावरण शांत होता है। लेकिन यदि काम का भार पड़ जाता है तो दिन-रात किसी भी वक्त लिख लेती हूं। ‘कालिंदी’ को मैंने रात में भी लिखा और दिन भी में भी। एकांत में लिखना मुझे अच्छा लगता है।
प्रश्न : एक कहानी को आप कितनी बैठकों या सीटिंग में पूरा कर लेती हैं और लगातार कितनी देर तक लिखती हैं ?
उत्तर : पहले मैं मन में एक खाका बनाती हूं। फिर उसे कागज पर उतारती हूं। खाका बनाकर रफ लिखती हूं। हमेशा हाथ से लिखती हूं। यहां तक कि अंतिम आलेख तक भी हाथ से ही लिखकर छपने भेजती हूं। एक कहानी लिखने में मुझे पन्द्रह-बीस दिन लग जाते हैं। कम-से-कम दस-पन्द्रह दिन तो लगते ही हैं। लिखास लगती है तो लिखती हूं। मैंने दस-बारह सदस्यों के परिवार में भी लिखा है और जब बच्चे छोटे थे तब भी खूब लिखा। मेरे जीवन में कोई नाटकीय मोड़ नहीं है। मैं कभी बिस्तर पर बैठकर लिखती हूं तो कभी आंगन में चारपाई पर लिख लेती हूं तो कभी सोफे पर बैठकर ही लिख लेती हूं।
प्रश्न : हिन्दी का लेखन हमारे यहां अपेक्षाकृत अर्थाभाव का शिकार होता है। केवल लेखन के बल पर समाज में सम्मानजनक ढंग से जीवन यापन करना कल्पनातीत है। यदि आप शुरू से केवल लेखन से जीविका अर्जित करतीं तो क्या अपने वर्तमान स्तर को बनाए रख सकती थीं ?
उत्तर : मैं अपने लेखन के बल पर ही जीवित हूं। और एकदम स्वावलम्बी हूं। मैं मानती हूं कोई भी लेखक अपने लेखन के बल पर ही जीविका चलाकर सम्मानजनक ढंग से समाज में जीवनयापन कर सकता है, बशर्ते उसकी कलम में दम हो। कलम कमजोर है तो आमदनी भी कमजोर होगी।
प्रश्न : आमतौर से लेखन और परिवार दो विरोधाभासी चीजें मानी जाती रही हैं। आपके लेखन में परिवार आडे़ आया या उससे लेखन में मदद मिलती रही ?
उत्तर : मेरे लेखन में परिवार एक क्षण के लिए कभी भी आड़े नहीं आया। जब तक मेरे पति जीवित रहे, उन्होंने मुझे लेखन के लिए बराबर प्रोत्साहित किया। उनको मेरे लेखन पर गर्व था। मैं तब कोई भी रचना किसी भी पत्र-पत्रिका अथवा प्रेस में उनके पढ़े बिना नहीं भेजती थी। जब कभी मेरी किसी रचना में कोई व्यक्तित्व अथवा चरित्र उजागर होता है तो कहते-ऐसा न करो। वे मेरे एकमात्र सच्चे आलोचक थे। उनकी हिन्दी भी बहुत अच्छी थी। कभी मैं अपनी रचना उन्हें पढ़कर सुना दिया करती थी और कभी वे स्वयं पढ़कर आवश्यक सुझाव दे दिया करते थे।
प्रश्न : आपकी कौन-सी कृति सर्वाधिक चर्चित रही और सबसे अधिक आमदनी किस रचना से आपको हुई ?
उत्तर : ‘कृष्णकली’। अब तक उसके दस से अधिक संस्करण हो चुके हैं। यह पुस्तक देश के अनेक विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में लगी हुई है। जहाँ तक आमदनी का सवाल है, कोई पैसा दे देता है कोई पूछता भी नहीं। इस हालत में ठीक-ठीक बता पाना मुश्किल है कि किस रचना से कितनी आमदनी हुई। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि पाठकों से मुझे जो स्नेह मिला वह पैसे की तुलना में कहीं अधिक रहा है। रचना छपने पर पाठकों के ढेरों पत्र तो आते ही हैं, बल्कि कभी-कभी तो कोई पाठक स्नेह से अभिभूत होकर कोई वस्तु तक उपहार में भेज देता है। ऐसे ही एक बार मेरी किसी रचना को पढ़कर बिहार से एक प्रशंसक ने आम का एक पार्सल भेजा था। और मजे की बात यह कि उसने प्रेषक का नाम तक नहीं लिखा था। मैंने उसे धन्यवाद प्रेषित करने के लिए उसका पता-ठिकाना ढूंढ़ने की बहुत कोशिश की, किन्तु निर्रथक रही। लेकिन सबसे विचित्र अनुभव तो मुझे अपने स्नेही पाठकों का उस दिन हुआ था जब एक व्यक्ति, जो बेहद मामूली से कपड़े पहने था, शुद्ध घी का एक कनस्तर लेकर हमारे दरवाजे पर आया और पूछने पर जब मैंने बताया कि मैं ही शिवानी हूं, तो बोला, ‘‘मैं आपके लिए अपने घर से शुद्ध घी लाया हूं। आप बहुत अच्छा लिखती हैं।’’
घुटनों तक मैली-सी धोती और वैसी ही कमीज में निपट देहाती दिखने वाले उस पाठक को मैंने बहुत समझाया-बुझाया कि घी वापस ले जाओ लेकिन वह एक न माना और जब वह दरवाजे से बिना घी दिए टस-से-मस नहीं हुआ तो उसकी श्रद्धा का सम्मान करने के उद्देश्य से मैंने भरे हुए कनस्तर से पूजा के पात्र में थोड़ा-सा घी लेकर किसी तरह से उसे निराश न करते हुए विदा किया।
प्रश्न : देखने-सुनने में आता है कि लेखक की किसी एक रचना पर पाठक प्रतिक्रियास्वरूप उसे सूचित करता है कि आपने तो हू-ब-हू मेरा चरित्र उतार दिया है या अमुक चरित्र में मैं हूं या फलां चरित्र मेरा सगा-संबंधी या परिचित है। इसके अतिरिक्त इसके विपरीत भी झेलना पड़ता है, जब कभी कोई सिरफिरा रचना पढ़ते ही लड़ने-मरने को तैयार हो जाता है। अदालत का दरवाजा खटखटाने की धमकी दे देता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी घटा है ?
उत्तर : वैसे तो पाठक अकसर रचना पढ़कर पत्र भेजते रहते हैं कि आपने अमुक-अमुक व्यक्ति का चरित्र हू-ब-हू उतारा है। ऐसा इसलिए होता है कि मेरे पात्र वास्तविक घटनाओं से ही होते हैं। लेकिन एक बार एक कहानी छपने पर सचमुच मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। 1970 में ‘धर्मयुग’ में मेरी ‘हंसा जाई अकेला’ नाम की कहानी छपी। यह कहानी नाथद्वारा (राजस्थान) के एक महंत पर आधारित थी। कहानी छपते ही उनके चेलों ने हायतोबा मचा दी। मुकदमा करने तक की धमकी देने लगे। ‘धर्मयुग’ के तत्कालीन संपादक डॉ. धर्मवीर भारती को भी उन्होंने धमकी-भरे पत्र लिखे। भारती जी ने परेशान होकर मुझे लिखा। लेकिन मेरे पास प्रमाण था। मैंने उस सम्बन्ध में एक चित्र लाकर भारती जी को भेज दिया। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। स्पष्ट था कि भारती जी ने प्रमाणस्वरूप वह चित्र महंत के चेलों को दिखाया होगा, जिससे उनकी बोलती बंद हो गई होगी।
प्रश्न : क्या आप एक समय एक ही रचना पर कार्य करती हैं या एकाधिक विषयों पर काम करती रहती हैं ?
उत्तर : मैं जब एक चीज पर लिखना शुरू करती हूं तो उसे समाप्त करने के पश्चात् ही दूसरी चीज लिखना शुरू करती हूं। फिर एक चीज समाप्त करने के बाद कुछ दिन तक नहीं लिखती। उन दिनों लिखती हूं, लेकिन कहानी उपन्यास नहीं, बल्कि निबंध अथवा लेख-आलेख आदि लिखती हूं। मैं समझती हूं कि एक समय में एक से अधिक रचनाओं पर काम करने से ध्यान बंट जाता है। और रचना में वह खूबसूरती नहीं आ पाती जो कि आनी चाहिए।
प्रश्न : अक्सर व्यक्ति किसी घटना विशेष के कारण लेखक, कवि या साहित्यसर्जक बन जाते हैं। आपके लेखिका बनने के पीछे क्या कारण रहा है ?
उत्तर : जैसा कि मैं पहले कहती आई हूं कि हमारे परिवार का वातावरण मेरे लेखिका बनने के सर्वथा उपयुक्त था। फिर मैं नौ वर्ष शांति निकेतन में गुरुदेव के संरक्षण में रही इसका भी मुझ पर प्रभाव पड़ा। लिखने के प्रति मेरा रुझान बचपन से ही था। यों कह सकते हैं कि मेरे अंदर लेखिका बनने का बीज मौजूद था, और उपयुक्त वातावरण मिलने पर मैं लेखिका बन गई। मैं नहीं मानती कि कोई घटना से प्रभावित होकर लेखक बन सकता है। उदाहरण के लिए किसी प्रियजन की मृत्यु से दुःखी होकर कोई संन्यासी तो बन सकता है, किन्तु लेखक नहीं बन सकता।
(दुर्गाप्रसाद नौटियाल से बातचीत)
वाग्देवी का अद्भुत वरदान
अपनी पटना-यात्रा के दौरान मेरी भेंट बिहार की
एक ऐसी प्रतिभाशाली महिला से हुई, जिन्हें देखकर सहज में विश्वास नहीं होता
है कि यह वही विलक्षण स्वरसाधिका हैं, जिन्हें बिहार के लोकगीतों का
चलता-फिरता विश्वकोश कहा गया है। मैं बहुत वर्षों से उनके मधुर सहज कण्ठ की
प्रशंसिका रही हूँ, किन्तु उन्हें कभी देखा नहीं था। मैं जहाँ ठहरी थी वहाँ
से उनका निवासस्थान निकट ही था, इसी से मैंने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट
की। मेरी मेजबान ने उन्हें मेरा सन्देश भिजवाया तो वे स्वयं आ गईं। मैं
उनके कंठ की प्रशंसिका थी और वे मेरी लेखनी की। मैंने जब उन्हें देखा तो
दंग रह गई। अत्यन्त साधारणसी वेशभूषा, सीधे पल्ले की साड़ी, उदास-सा चेहरा
किन्तु जब हँसी तो वहीं सरल चेहरा एक क्षण में उद्भासित हो उठा।
निश्चय ही बिहार को अपनी इस स्वरसाधिका पर गर्व होना चाहिए। अथक परिश्रम से ही उन्होंने बिहार के लोकगीतों का जैसा अद्भुत संकलन किया है, वह स्वयं अपने में मिसाल है। शायद ही कोई क्षेत्रीय लोकधुन या संस्कार गीत उनके कंठ में न रिसा हो। वास्तव में ये भारत की रेशमा हैं-वही सरलता, वही निरभिमान सहज स्मित और मांसल कंठ की वही जादूगरी। अन्तर इतना ही है कि पाकिस्तान ने रेशमा-रत्न को गुदड़ी से निकाल खरे सोने से चौखट में मढ़ दिया है और हमारे भारत की ये रेशमा अभी भी अपने काष्ठ के चौखट में ही सन्तुष्ट हैं।
स्वर्गीय जगत बहादुर सिंह की पुत्री, विंध्यवासिनी का जन्म 5 मार्च, 1920 को मुजफ्फरपुर में हुआ। जन्म के बाद ही ये मातृहीन हो गईं, अपने नाना चतुर्भुज सहाय की देखरेख में उनकी शिक्षा प्रारम्भ हुई। भगवान भक्त नाना हरिभजन गाने में ही लीन रहते थे, वही विंध्यवासिनी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। इनका मधुर कंठ सुन नाना ने इन्हें क्षितीशचन्द्र वर्मा से संगीत-शिक्षा दिलवाई किन्तु स्कूली शिक्षा अधिक नहीं हो पाई।
यह भी एक विचित्र संयोग था कि 1931 में इनका विवाह श्री सहदेवेश्वर वर्मा (अब स्वर्गीय) से हुआ जिन्होंने इन्हें साहित्य एवं संगीत के अध्ययनगायन की सम्पूर्ण सुविधाएँ दिला दीं। 1942 में स्थायी रूप से पटना रहने आ गईं और यहाँ एक कन्या विद्यालय में संगीत शिक्षिका बन गईं। इसी बीच, उदार पति के सहयोग से इन्होंने प्रयाग से विशारद और हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से साहित्य विभूषण की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर लीं। पति स्वयं संगीतज्ञ थे, उन्हीं के प्रयास से इन्होंने भातखण्डे संगीत विद्यालय, लखनऊ, से शास्त्रीय संगीत की भी विधिवत् शिक्षा प्राप्त की।
अपने पति के सहयोग से ही इन्होंने 1949 में 'विंध्यकला मन्दिर, पटना' की स्थापना की। यह बिहार का एक प्रमुख लोकगीत, लोकनृत्य एवं नाट्य के साथ-साथ शास्त्रीय संगीत विद्यापीठ भी है। श्री मकबूल नदाफ लिखते हैं, “यह कला मन्दिर, विंध्यवासिनी देवी का ही मानस-पुत्र है, रवि वाबू ने जब प्रारम्भ में बँगला रंगमंच पर महिलाओं को उतारा था तब उनकी कड़ी आलोचना की गई थी, किन्तु इन सारी आलोचनाओं के बावजूद रवि बाबू बँगला लोक रंगमंच को विकसित करते रहे। समय के साथ-साथ स्थिति बदली और बाद में उनकी प्रशंसा होने लगी। 30 वर्ष के पश्चात् उसी ‘अमृत बाजार' में श्री तुषारकान्ति घोष ने लिखा कि रवि बाबू ने बँगला रंगमंच को उठाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने बंग जनजीवन में लोकसंगीत और लोकनृत्य को भी उभार दिया, यही बात बहुत कुछ अंश में विंध्यवासिनी देवी जी पर विहार के लिए भी लागू होती है।”
विंध्यवासिनी देवी के विचार में बिहार में जब तक ऐसे रंगमंच का निर्माण नहीं होता, जिसके माध्यम से बिहार की बहू-बेटियों को संगीत, नृत्य और अभिनय की शिक्षा दी जा सके, बिहार की संस्कृति का अध्याय अधूरा ही कहलाएगा। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि कला जनजीवन को उठाती है, गिराती नहीं है। इसी विश्वास से उन्होंने 1948 में 'मानव' नामक संगीत रूपक से प्रभूत प्रशंसा अर्जित की। लोकगीतों और लोकनृत्यों से सँवारा यह रूपक, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत होकर अनेक अवसरों पर मंचित किया जा चुका है। तत्कालीन लोकसंस्कृति निदेशक श्री गोरखनाथ सिंह ने 'मानव' देखकर कहा था कि “जो कार्य शहनाईनवाज श्री बिस्मिल्ला खान ने किया, वही कार्य विंध्यवासिनी देवी ने लोकगीतों के लिए किया।” वास्तव में देखा जाए तो बिहार की गुदड़ी में छिपे इस अनूठे रत्न को पहचानने का श्रेय स्व. श्री जगदीशचन्द्र माथुर को है, उन्होंने आकाशवाणी के महानिदेशक होने पर, अनेक अनावश्यक बाधाओं और औपचारिकताओं को लाँघ, उन्हें पटना आकाशवाणी केन्द्र के लोकगीतों की संयोजिका के पद पर नियुक्त किया और उस पद पर वे पूर्ण निष्ठा से 1979 तक कार्यरत रहीं।
संप्रति, पटना केन्द्र के संयोजिका पद से सेवानिवृत्त हो ये अपना समस्त समय अपने साधना केन्द्र को सुप्रतिष्ठित करने में लगा रही हैं। साथ ही राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनेक अवसरों पर वे लोकसंगीत के कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रस्तुत करती रहती हैं।
बारह भागों में 'लोकसंगीत सागर' के प्रथम भाग ‘सोहर प्रकरण' को उन्होंने बिहार सरकार के जनसम्पर्क विभाग को प्रकाशनार्थ दिया है। रामायण काल से आधुनिक काल तक के इतिहास पर आधारित नोटेशन सहित एक अन्य कृति 'वैशाली महिमा' तथा भोजपुरी, मगही एवं मैथिली के ‘लोकगीतों की रचना' भी प्रकाशनाधीन है।
यही नहीं, लोकशब्दों का एक बृहतकोश लोकशब्द सागर-सम्पादिका विंध्यवासिनी देवी, सहायक सम्पादक (संतोष कुमार सिन्हा) भी ऐसा एक अद्भुत समृद्ध कोश है जिसमें लगभग दस हजार लोकशब्दों का संकलन है। इसमें मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका एवं वज्जिका लोकशब्दों का भाषाविज्ञान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है।
इसके अतिरिक्त उनके पास बिहार के लोकजीवन की जो दुर्लभ सामग्री उपलब्ध है, उससे दर्जनों ग्रंथों की सृष्टि हो सकती है। उनके विषय में यह उक्ति सर्वथा सटीक बैठती है कि कलाकार की महान् कला से ही अलंकार भी अलंकृत होता है।
अपने इन्हीं गुणों के कारण वे 7 वर्षों की सुदीर्घ अवधि तक भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी की मानद सदस्या रह चुकी हैं। स्वर्गीय पं. जवाहरलाल नेहरू के जीवन के अंतिम काल तक गणतन्त्र दिवस आदि राष्ट्रीय उत्सवों में उन्होंने सदैव बिहार के सांस्कृतिक दल का चुनाव किया।
इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय फिल्मों में लोकधुन देने के साथ-साथ, एक मैथिली फिल्म 'कन्यादान' में इन्होंने स्वतन्त्र रूप से संगीत-निर्देशन भी किया। भोजपुरी फिल्म में वे पार्श्वगायिका भी रहीं। इनके कंठमाधुर्य से प्रभावित होकर, 'हिजमास्टर्स वायस' ने इनके गाए संस्कार गीतों का एक रेकार्ड भी तैयार किया। हिन्दी फिल्म 'छठ मइया की महिमा' में डॉ. भूपेन्द्र हजारिका के संगीत-निर्देशन में पार्श्वगायिका के रूप में इन्होंने चार गीत गाकर अभूतपूर्व लोकप्रियता अर्जित की।
भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् की ओर से वे दो बार मारीशस गईं। यहाँ स्वदेशी लोकगीतों की क्षुधा से क्षुधातुर अनेकानेक प्रवासी भारतीयों के संस्कृति शुष्क जीवन में इन्होंने जो रसवृष्टि की, वह सदा उनके लिए स्मरणीय रहेगी–मैथिली, मगही, भोजपुरी भाषाओं में जन्म, विवाह गीत गाने में समान रूप से समर्थ इस स्वरसाधिका को निश्चय ही विधाता का वरदान है।
1947 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से विभूषित किया, इसके अतिरिक्त अनेक ताम्रपत्र. पदक प्राप्त हए। एक साधिका के रूप में इनका जीवन अनेक संघर्षों से जूझते ही व्यतीत हुआ है, पति का निधन इनके लिए ऐसा आघात सिद्ध हुआ, जिससे वह टूट-सी गईं किन्तु इनका लौह व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जो टूटकर भी बिखरता नहीं।
मेरे पास बैठकर अस्वस्थ होने पर भी मेरे अनुरोध पर उन्होंने कितने ही सुमधुर गीत गाकर सुनाए, एक-के-बाद-एक, जैसे किसी झरने की हीरक जलधार मुझे आपादमस्तक रससक्ति करती रही। परिशीलित सुरीले कंठ की स्वामिनी विंध्यवासिनी देवी की गायन भंगिमा की चिन्ताशीलता एवं रसबोध समान रूप से सुपरिस्फुट है।
वह विवाह-गीत हो या सोहर या विद्यापति की कोई लोकप्रिय रचना, इस गायिका का सम्पूर्ण निवेदन ही है-अद्भुत व्यंजनामय एवं हृदयस्पर्शी। ऐसी शिल्पबोधसम्पन्नता केवल रियाज से ही नहीं आती, वह स्वयं वाग्देवी का वरदान होता है। उनके दीप्त-सतेज कंठ को किसी माइक की आवश्यकता कभी नहीं रहती, सरलता ऐसी कि कहीं भी कोई विवाह हो या पुत्र-जन्म, उनसे अनुरोध किया और वे चटपट गाकर आयोजन को धन्य कर देती हैं।
मैंने जब उनसे कहा कि आप जैसी विलक्षण महिला के विषय में कुछ लिखना चाहती हूँ तो उन्होंने हँसकर कहा, 'मुझ पर क्या लिखोगी बहन! देख तो रही हो, मैं तो एक अत्यन्त साधारण गृहिणी मात्र हूँ।"
विधाता ऐसी विलक्षण गृहिणी के सुमधुर कंठ को सुदीर्घ जीवन दे और स्वयं अपनी ही प्रतिभा से सर्वथा अनभिज्ञ यह वन-कोकिला निरन्तर भारत के आम्रकुंजों में टहूकती रहे।
निश्चय ही बिहार को अपनी इस स्वरसाधिका पर गर्व होना चाहिए। अथक परिश्रम से ही उन्होंने बिहार के लोकगीतों का जैसा अद्भुत संकलन किया है, वह स्वयं अपने में मिसाल है। शायद ही कोई क्षेत्रीय लोकधुन या संस्कार गीत उनके कंठ में न रिसा हो। वास्तव में ये भारत की रेशमा हैं-वही सरलता, वही निरभिमान सहज स्मित और मांसल कंठ की वही जादूगरी। अन्तर इतना ही है कि पाकिस्तान ने रेशमा-रत्न को गुदड़ी से निकाल खरे सोने से चौखट में मढ़ दिया है और हमारे भारत की ये रेशमा अभी भी अपने काष्ठ के चौखट में ही सन्तुष्ट हैं।
स्वर्गीय जगत बहादुर सिंह की पुत्री, विंध्यवासिनी का जन्म 5 मार्च, 1920 को मुजफ्फरपुर में हुआ। जन्म के बाद ही ये मातृहीन हो गईं, अपने नाना चतुर्भुज सहाय की देखरेख में उनकी शिक्षा प्रारम्भ हुई। भगवान भक्त नाना हरिभजन गाने में ही लीन रहते थे, वही विंध्यवासिनी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। इनका मधुर कंठ सुन नाना ने इन्हें क्षितीशचन्द्र वर्मा से संगीत-शिक्षा दिलवाई किन्तु स्कूली शिक्षा अधिक नहीं हो पाई।
यह भी एक विचित्र संयोग था कि 1931 में इनका विवाह श्री सहदेवेश्वर वर्मा (अब स्वर्गीय) से हुआ जिन्होंने इन्हें साहित्य एवं संगीत के अध्ययनगायन की सम्पूर्ण सुविधाएँ दिला दीं। 1942 में स्थायी रूप से पटना रहने आ गईं और यहाँ एक कन्या विद्यालय में संगीत शिक्षिका बन गईं। इसी बीच, उदार पति के सहयोग से इन्होंने प्रयाग से विशारद और हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से साहित्य विभूषण की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर लीं। पति स्वयं संगीतज्ञ थे, उन्हीं के प्रयास से इन्होंने भातखण्डे संगीत विद्यालय, लखनऊ, से शास्त्रीय संगीत की भी विधिवत् शिक्षा प्राप्त की।
अपने पति के सहयोग से ही इन्होंने 1949 में 'विंध्यकला मन्दिर, पटना' की स्थापना की। यह बिहार का एक प्रमुख लोकगीत, लोकनृत्य एवं नाट्य के साथ-साथ शास्त्रीय संगीत विद्यापीठ भी है। श्री मकबूल नदाफ लिखते हैं, “यह कला मन्दिर, विंध्यवासिनी देवी का ही मानस-पुत्र है, रवि वाबू ने जब प्रारम्भ में बँगला रंगमंच पर महिलाओं को उतारा था तब उनकी कड़ी आलोचना की गई थी, किन्तु इन सारी आलोचनाओं के बावजूद रवि बाबू बँगला लोक रंगमंच को विकसित करते रहे। समय के साथ-साथ स्थिति बदली और बाद में उनकी प्रशंसा होने लगी। 30 वर्ष के पश्चात् उसी ‘अमृत बाजार' में श्री तुषारकान्ति घोष ने लिखा कि रवि बाबू ने बँगला रंगमंच को उठाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने बंग जनजीवन में लोकसंगीत और लोकनृत्य को भी उभार दिया, यही बात बहुत कुछ अंश में विंध्यवासिनी देवी जी पर विहार के लिए भी लागू होती है।”
विंध्यवासिनी देवी के विचार में बिहार में जब तक ऐसे रंगमंच का निर्माण नहीं होता, जिसके माध्यम से बिहार की बहू-बेटियों को संगीत, नृत्य और अभिनय की शिक्षा दी जा सके, बिहार की संस्कृति का अध्याय अधूरा ही कहलाएगा। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि कला जनजीवन को उठाती है, गिराती नहीं है। इसी विश्वास से उन्होंने 1948 में 'मानव' नामक संगीत रूपक से प्रभूत प्रशंसा अर्जित की। लोकगीतों और लोकनृत्यों से सँवारा यह रूपक, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत होकर अनेक अवसरों पर मंचित किया जा चुका है। तत्कालीन लोकसंस्कृति निदेशक श्री गोरखनाथ सिंह ने 'मानव' देखकर कहा था कि “जो कार्य शहनाईनवाज श्री बिस्मिल्ला खान ने किया, वही कार्य विंध्यवासिनी देवी ने लोकगीतों के लिए किया।” वास्तव में देखा जाए तो बिहार की गुदड़ी में छिपे इस अनूठे रत्न को पहचानने का श्रेय स्व. श्री जगदीशचन्द्र माथुर को है, उन्होंने आकाशवाणी के महानिदेशक होने पर, अनेक अनावश्यक बाधाओं और औपचारिकताओं को लाँघ, उन्हें पटना आकाशवाणी केन्द्र के लोकगीतों की संयोजिका के पद पर नियुक्त किया और उस पद पर वे पूर्ण निष्ठा से 1979 तक कार्यरत रहीं।
संप्रति, पटना केन्द्र के संयोजिका पद से सेवानिवृत्त हो ये अपना समस्त समय अपने साधना केन्द्र को सुप्रतिष्ठित करने में लगा रही हैं। साथ ही राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनेक अवसरों पर वे लोकसंगीत के कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रस्तुत करती रहती हैं।
बारह भागों में 'लोकसंगीत सागर' के प्रथम भाग ‘सोहर प्रकरण' को उन्होंने बिहार सरकार के जनसम्पर्क विभाग को प्रकाशनार्थ दिया है। रामायण काल से आधुनिक काल तक के इतिहास पर आधारित नोटेशन सहित एक अन्य कृति 'वैशाली महिमा' तथा भोजपुरी, मगही एवं मैथिली के ‘लोकगीतों की रचना' भी प्रकाशनाधीन है।
यही नहीं, लोकशब्दों का एक बृहतकोश लोकशब्द सागर-सम्पादिका विंध्यवासिनी देवी, सहायक सम्पादक (संतोष कुमार सिन्हा) भी ऐसा एक अद्भुत समृद्ध कोश है जिसमें लगभग दस हजार लोकशब्दों का संकलन है। इसमें मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका एवं वज्जिका लोकशब्दों का भाषाविज्ञान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है।
इसके अतिरिक्त उनके पास बिहार के लोकजीवन की जो दुर्लभ सामग्री उपलब्ध है, उससे दर्जनों ग्रंथों की सृष्टि हो सकती है। उनके विषय में यह उक्ति सर्वथा सटीक बैठती है कि कलाकार की महान् कला से ही अलंकार भी अलंकृत होता है।
अपने इन्हीं गुणों के कारण वे 7 वर्षों की सुदीर्घ अवधि तक भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी की मानद सदस्या रह चुकी हैं। स्वर्गीय पं. जवाहरलाल नेहरू के जीवन के अंतिम काल तक गणतन्त्र दिवस आदि राष्ट्रीय उत्सवों में उन्होंने सदैव बिहार के सांस्कृतिक दल का चुनाव किया।
इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय फिल्मों में लोकधुन देने के साथ-साथ, एक मैथिली फिल्म 'कन्यादान' में इन्होंने स्वतन्त्र रूप से संगीत-निर्देशन भी किया। भोजपुरी फिल्म में वे पार्श्वगायिका भी रहीं। इनके कंठमाधुर्य से प्रभावित होकर, 'हिजमास्टर्स वायस' ने इनके गाए संस्कार गीतों का एक रेकार्ड भी तैयार किया। हिन्दी फिल्म 'छठ मइया की महिमा' में डॉ. भूपेन्द्र हजारिका के संगीत-निर्देशन में पार्श्वगायिका के रूप में इन्होंने चार गीत गाकर अभूतपूर्व लोकप्रियता अर्जित की।
भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् की ओर से वे दो बार मारीशस गईं। यहाँ स्वदेशी लोकगीतों की क्षुधा से क्षुधातुर अनेकानेक प्रवासी भारतीयों के संस्कृति शुष्क जीवन में इन्होंने जो रसवृष्टि की, वह सदा उनके लिए स्मरणीय रहेगी–मैथिली, मगही, भोजपुरी भाषाओं में जन्म, विवाह गीत गाने में समान रूप से समर्थ इस स्वरसाधिका को निश्चय ही विधाता का वरदान है।
1947 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से विभूषित किया, इसके अतिरिक्त अनेक ताम्रपत्र. पदक प्राप्त हए। एक साधिका के रूप में इनका जीवन अनेक संघर्षों से जूझते ही व्यतीत हुआ है, पति का निधन इनके लिए ऐसा आघात सिद्ध हुआ, जिससे वह टूट-सी गईं किन्तु इनका लौह व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जो टूटकर भी बिखरता नहीं।
मेरे पास बैठकर अस्वस्थ होने पर भी मेरे अनुरोध पर उन्होंने कितने ही सुमधुर गीत गाकर सुनाए, एक-के-बाद-एक, जैसे किसी झरने की हीरक जलधार मुझे आपादमस्तक रससक्ति करती रही। परिशीलित सुरीले कंठ की स्वामिनी विंध्यवासिनी देवी की गायन भंगिमा की चिन्ताशीलता एवं रसबोध समान रूप से सुपरिस्फुट है।
वह विवाह-गीत हो या सोहर या विद्यापति की कोई लोकप्रिय रचना, इस गायिका का सम्पूर्ण निवेदन ही है-अद्भुत व्यंजनामय एवं हृदयस्पर्शी। ऐसी शिल्पबोधसम्पन्नता केवल रियाज से ही नहीं आती, वह स्वयं वाग्देवी का वरदान होता है। उनके दीप्त-सतेज कंठ को किसी माइक की आवश्यकता कभी नहीं रहती, सरलता ऐसी कि कहीं भी कोई विवाह हो या पुत्र-जन्म, उनसे अनुरोध किया और वे चटपट गाकर आयोजन को धन्य कर देती हैं।
मैंने जब उनसे कहा कि आप जैसी विलक्षण महिला के विषय में कुछ लिखना चाहती हूँ तो उन्होंने हँसकर कहा, 'मुझ पर क्या लिखोगी बहन! देख तो रही हो, मैं तो एक अत्यन्त साधारण गृहिणी मात्र हूँ।"
विधाता ऐसी विलक्षण गृहिणी के सुमधुर कंठ को सुदीर्घ जीवन दे और स्वयं अपनी ही प्रतिभा से सर्वथा अनभिज्ञ यह वन-कोकिला निरन्तर भारत के आम्रकुंजों में टहूकती रहे।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i 






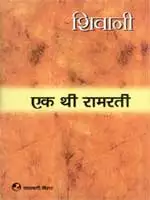


_s.jpg)
