|
नारी विमर्श >> भैरवी (अजिल्द) भैरवी (अजिल्द)शिवानी
|
358 पाठक हैं |
|||||||
पति-व्रता स्त्री के जीवन पर आधारित उपन्यास
अवकाश की नीलिमा मानो उस अरण्य को चीरती हुई झपाटे से नीचे उतर आई थी।
प्राचीन वट और अश्वत्थ के धूमिल वृक्ष मौन साधकों की तरह अचल खड़े थे। वह उस
खुली खिड़की से, बड़ी देर से इन्हीं वृक्षों को देख रही थी। क्या इन वृक्षों
की पत्तियाँ भी, अरण्य की मूल भयावहता से सहमकर हिलना भूल गई थीं? उसने करवट
बदलने की कोशिश की। जरा हिली कि रग-रग में दर्द दौड़ गया। वह कराह उठी। उस
दिन सिसकी में डूबे हुए करुण निःश्वास को सुनकर, कोठरी के किसी अँधेरे कोने
पर लगी खटिया से कूदकर थुलथुले बदनवाली एक प्रौढ़ा उसके चेहरे पर झुक गई।
'जय गुरु, जय गुरु' की रट लगाते हुए वह प्रौढ़ा अपना चेहरा, उसके इतने निकट
ले आई कि जर्दा-किकाम की महक, किसी तेज गन्धवाली अगर की धूनी की याद ताजा
करते हुए, उसकी सुप्त चेतना को झकझोर गई। उसने सहमकर आँखें मूंद लीं। बेहोशी
का बहाना बनाए वह लेटी ही रही। प्रौढ़ा संन्यासिनी बड़बड़ाती हुई एक बार फिर
अपने अन्धकारपूर्ण कोने में खो गई।
ओफ, कैसी भयावह आकृति थी उस संन्यासिनी की! ऊँची बँधी गेरुआ मर्दाना धोती,
जिसे उसने घुटनों तक खींचकर, कमर की विराट परिधि में ही आँचल से लपेटकर बाँध
लिया था। परतों में झूल रहे, नग्न उदर से लेकर, तुम्बी-से बन्धनहीन लटके
स्तनों तक रक्त-चन्दन का प्रगाढ़ लेप, जिसकी रक्तिम आभा उसके रूखे खुरदरे
चेहरे को भी ललछौंहा बना गई थी। एक तो मेरुदंड की असह्य वेदना, उस पर
संन्यासिनी की वह रौद्रमूर्ति। उसने आँख बन्द कर लीं, पर कब तक वास्तविकता से
ऐसे आँखें मूंदे अचेत पड़ी रहेगी? क्या जीवन-भर उसे ऐसी ही भयावह भगवा
मूर्तियों के बीच अपनी पंगु अवस्था बितानी होगी? और फिर उस भयानक कालकोठरी की
अमानवीय निस्तब्धता ही उसका गला घोंट देने के लिए पर्याप्त थी। देखा जाए तो
वह कोठरी थी ही कहाँ, किसी मालगाड़ी के बन्द डिब्बे-सी सँकरी गुफा थी, जिसकी
एक दीवार को तोड़-फोड़कर एक नन्ही-सी टेढ़ी खिड़की बना दी गई थी। खिड़की भी
ऐसी कि कभी अपने बंकिम गवाक्ष से मुट्टी-भर ताजी हवा का झोंका लाती भी, तो
दूसरे ही क्षण उसी तत्परता से, फटाफट अपने अनाड़ी जर्जर पट मूंदकर, दूसरे
झोंके का पथ, स्वयं ही अवरुद्ध भी कर देती। कभी-कभी कोने में जल रही धूनी के
धुएँ की कड़वी दुर्गन्ध से उसका दम घुटने लगता, चन्दन के जी में आता कि वह
भागकर बाहर चली जाए, पर भागेगी कैसे?
उस दिन, विवशता की सिसकी उस गुहा की नीची, झुक झुक आती छत से टकराकर,
गुरुगर्जना-सी गूंज उठी थी, और वह चंडिका-सी वैष्णवी, उसके कुम्हलाए आँसुओं
से भीगे चहरे पर एक बार फिर झुककर बाहर भाग गई। थोड़ी ही देर में कई कंठों का
गुंजन, उसके कानों से टकराने लगा, पर वह दाँत से दाँत मिलाए, आँखें बन्द किए
पड़ी रही। बादलों से अधढके दूज के चाँद का थका-हारा-सा प्रकाश उसके पीले
चेहरे पर फैला हुआ था। बड़े-बड़े मुँदे नयनों की कोर पर टपकी आँसुओं की
बूंदें गौर से देखने पर नजर आ ही जाती थीं।
"देखा न? होश में आ गई है, होश में न आई होती तो आँखों में आँसू आते? दो बार
तो मैंने इसे कराहते हुए सुना।" वही संन्यासिनी कहे जा रही थी, "मैं तो कहती
हूँ गुसाईं, कहीं भीतर भारीगुम चोट खा गई है, आज आठवाँ दिन है, पानी की एक
बूंद भी गले के नीचे नहीं उतरी-किसी की मोटर माँगकर इसे शहर के बड़े अस्पताल
में पहुँचा दो...।"
"नहीं!" नगाड़े पर पड़ती चोट-सा एक कठोर स्वर गूंज उठा, “यह मरेगी नहीं।" "जय
गुरु, जय गुरु!" संन्यासिनी कहने लगी, “गुरु का वचन क्या कभी मिथ्या हो सकता
है? ये लीजिए, चरन नई चिलम भरकर ले आई, आप विश्राम करें। मैं तो इसके पास
बैठी ही हूँ, जब आपने कह दिया कि यह नहीं मरेगी तब फिर हमें कोई डर नहीं
रहा।"
"क्यों री चरन, चिलम भरना भूल गई क्या?" गाँजे के दम से अवरुद्ध गुरु का स्वर
चरन से बेदम चिलम की कैफियत माँगने लगा।
“अरे भूलेगी कैसे, असल में इस ससुरी की हमने आज खूब पिटाई की है।" संन्यासिनी
ने अपनी चौड़ी हथेली, खटिया पर टिका दी।
"क्यों, आज क्या इसने फिर हमारी सप्तमी चुरा ली?"
“और क्या! गिनकर पाँच पुड़ियाँ धरी थीं। आज जब आपकी चिलम सजाने को ढूँढ़ने
लगी तो देखा तीन ही पुड़ियाँ हैं। हम समझ गईं। आखिर साँप का पैर तो साँप ही
चीन्हता है गुसाईं, हमने हरामजादी को उजाले में खींचकर आँखें देखीं तो एकदम
लाल जवाफूल। बस चोरी पकड़ ली। सत्रह की पूरी नहीं हुई और लगाएगी गाँजे का दम,
वह भी गुरु का गाँजा-बस तीन चिमटे ऐसे दिए कि पीठ पर गुरु का त्रिशूल उभर आया
है।"
"अच्छा, अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया, हाथ-वाथ चलाना ठीक नहीं है, माया!
चलो सो जाओ अब, हमें राघव ने बुलाया है, बर्दवान से कोई रामदासी कीर्तनिया
आया है-हम कल तक लौटेंगे।"
गुरु का कंठ-स्वर की सप्तमी के रंग में रंग गया था...।
खड़ाऊँ की क्रमशः विलीन होती खटखट से चन्दन आँखें बन्द होने पर भी गुरु के
विदा हो चुकने के सम्बन्ध में आश्वस्त हो सकी। वैष्णवी उठी, और उसके उठते ही
उसकी देह-गरिमा से एक कोने को झूला-सी बन गई मूंज की खटिया, एक बार फिर अपना
सन्तुलन लौटा लाई। अब तक नीचे अतल जल में डूबती हलकी पोटली-सी ही चन्दन सहसा
ऊपर उठ आई। थोड़ी ही देर में, कोने की खटिया से वैष्णवी के नासिका-गर्जन से
आश्वस्त होकर उसने आँखें खोल लीं। गगन की धृष्टा चाँदनी, अब पूरे कमरे में
रेंगती फैल गई थी। कृपण वातायन से घुस आया हवा का एक उदार झोंका उसे चैतन्य
बना गया। पहली बार, अनुसन्धानी दृष्टि फेर-फेरकर उसने पूरे कमरे को ठीक से
देखा। कितनी नीची छत थी! लगता था, हाथ बढ़ाते ही वह छत की बल्लियों को छ सकती
है। धुएँ से काली पड़ी हुई काठ की उन मोटी-मोटी बल्लियों के सहारे, कई गेरुआ
पोटलियाँ झूल रही थीं, खूटियों पर टँगी गेरुआ धोतियाँ, दो-तीन बड़े-बड़े
दानों की रुद्राक्ष-कंठियाँ और काले चिकने कमंडलों को देखकर, इतना समझने में
उसे विलम्ब नहीं हुआ कि वह वैरागियों की किसी बस्ती में आ गई। अचानक उसकी
भटकती दृष्टि कोने में गड़े एक लम्बे सिन्दूर-पुते त्रिशूल पर निबद्ध हो गई।
निर्वात दीप की शिखा हवा में झूम रही थी, त्रिशल पर लाल और सफेद चिथड़ों-सी
नन्हीं ध्वजाएँ फड़फड़ा रही थीं और ठीक त्रिशूल के नीचे पड़े थे, स्तूपीकृत
नरमुंड।
|
|||||


 i
i 






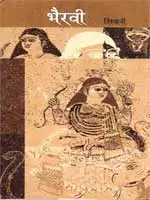


_s.jpg)
