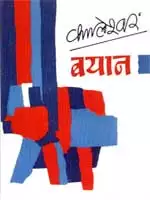|
कहानी संग्रह >> बयान बयानकमलेश्वर
|
56 पाठक हैं |
|||||||
कमलेश्वर की कुछ चुनी हुई कहानियों का संग्रह
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
इस संग्रह में बयान के साथ कमलेश्वर की वे सभी कहानियाँ संग्रहीत हैं
जिन्हे कहानीकार की विशिष्ट उपलब्धियों के रुप में सभी ने स्वीकारा और
सराहा है।
‘नई कहानी आंदोलन’ के प्रमुख प्रवर्तक प्रखर प्रवक्ता एक ‘समांतर लेखन’ आंदोलन के प्रथम-पुरुष के रुप में कमलेश्वर ने आम आदमी के साथ अपने लेखन को जोड़ा और अपनी रचनाओं में उसे सशक्त अभिव्यक्ति दी।
‘आजादी मुबारक’, ‘दस प्रतिनिधि कहानियाँ’, ‘राजा निरबंसिया’ ‘मांस का दरिया’, कस्बे का आजादी’, ‘खोई हुई दिशाएँ’, ‘जार्ज पंचम की नाक’, ‘मेरी प्रिय कहानियाँ’, ‘इतने अच्छे दिन’, ‘रावल की रेल’, ‘समग्र कहानियाँ’, के बाद ‘बयान’ कमलेश्वर द्वारा आम आदामी की अभिव्यक्ति की सशक्त सनद है।
‘नई कहानी आंदोलन’ के प्रमुख प्रवर्तक प्रखर प्रवक्ता एक ‘समांतर लेखन’ आंदोलन के प्रथम-पुरुष के रुप में कमलेश्वर ने आम आदमी के साथ अपने लेखन को जोड़ा और अपनी रचनाओं में उसे सशक्त अभिव्यक्ति दी।
‘आजादी मुबारक’, ‘दस प्रतिनिधि कहानियाँ’, ‘राजा निरबंसिया’ ‘मांस का दरिया’, कस्बे का आजादी’, ‘खोई हुई दिशाएँ’, ‘जार्ज पंचम की नाक’, ‘मेरी प्रिय कहानियाँ’, ‘इतने अच्छे दिन’, ‘रावल की रेल’, ‘समग्र कहानियाँ’, के बाद ‘बयान’ कमलेश्वर द्वारा आम आदामी की अभिव्यक्ति की सशक्त सनद है।
कहानियां जो भी हों, पर उनके प्रश्न और उत्तर नये हैं।
कहानी ने एक बार फिर अपनी मुक्ति का अहसास कराया है। अच्छा है कि यह
मुक्ति किसी आंदोलन का नाम अख्तियार नहीं कर रही है। आंदोलनों और
प्रतिआंदोलनों से ऊबी हुई कथा-चेतना अब अपनी दृष्टि सम्पन्नता के साथ ही
आत्मबोध से आप्लावित है।
कहानी का सबसे बड़ा संकट ही यह होता कि वह आत्मबोध और समयबोध को किस स्तर पर स्वीकृत करे। कथात्मकता के स्तर पर या कथ्य के बिंदु पर या लेखक के अपने बोध के तनाव पर ?
अगर इस स्थिति को जरा और स्पष्ट करलिया जाए तो बात इकहरी हो जाने का खतरा है। पर विवेचन की सरलता के लिए इन आसंगों को अलग कर लिया जाना बेहतर है।
कथात्मकता का निर्वाह कर सकने के लिए रचना क्षणों में लेखकीय चेतना मूड़ों, स्थितियों, घटनाओं क्षणों मनःस्थितियों का संयमित चुनाव करती चलती है, ताकि कथ्य का यथार्थ खण्डित न होने पाए और वह अपने ‘फॉर्म’ की रक्षा भी कर ले जाए या कि कथ्य को एक ‘फॉर्म’ दे पाए। फॉर्म का यह झमेला बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि यह इतना दबाव डालता है कि कभी-कभी कहानी वह नहीं बन पाती, जो उसकी नियति थी। कुछ लेखकों के लिए कथात्मकता नैरेटिव या स्ट्रक्चर का पर्याय है, कि कहानी का रूपबंध क्या है, कि उसकी विकास सरणी क्या है। सर्जनात्मक प्रतिभा के लिए यह बाहरी उपादन व्यर्थ होते हैं। सर्जनात्मक प्रतिभा अपनी कथात्मकता के लिए दूसरे दर्जे के यथार्थवादी वातावरण या तथ्यसम्मत सम्भावनाओं के व्यामोह में नहीं पड़ती। वह फ़ॉर्म की तलाश भी नहीं करती और न अपनी घटित स्थितियों के बयान के लिए होटलों नाचघरों या बिस्तरों के कोने खोजती है। बहुत दिनों तक फ़ॉर्म की रक्षा (एक तरह से) कहानी में लड़की की उपस्थिति करती रही। अगर कहानी में लड़की न होती तो मूड्स के टुकड़े जुड़ नहीं पाते, लड़की के बाद यह काम स्त्री की जाँघों से लिया जाने लगा।
और फिर, दो अंगुल जगह से। कुछ कोशिश आत्महत्या के तनाव को इस्तेमाल करके की गई। कभी-कभी मात्र सैक्स चित्रण के सहारे कहानी की गति को बरकरार रखा गया; और जहाँ वह सब नहीं मिला, वहीं कहानी पहले ही पैराग्राफ़ पर घुटने तोड़कर बैठ गई। यानी कहानी पढ़ी नहीं गई। पिछले दिनों का छपित साहित्य इसका प्रमाण है कि चीजें छपीं, पर पढ़ी नहीं गईं। साहित्यनिष्ठ लोग जैसे तैसे पढ़ते भी रहे, पर उनके मानस पर कुछ घटित नहीं हुआ। हुआ यह कि कथात्मकता की सार्थक भंगिमा को नये धरातल पर बहुतों ने आत्मसात नहीं कर पाया, अपने समय के दबाव-तनाव और विक्रिया को नहीं समझा। बहुतों को यही लगा कि कुछ भी बक दिया जाय, वह कहानी हो जायेगी। कहानी की ऊपरी सहजता ने एक मृगछलना का काम किया और कहानीकार हो सकने की प्यास में उस मृगछलना के पीछे दौड़ते-दौड़ते बहुत से बेहोश होकर गिर पड़े। बहुतों ने दम तोड़ दिया।
सवाल था कि कहानी की यह कहानीपरकता थी भी कहाँ ? यानी कहानी का अपना वह फॉर्म जो उसे अन्य विधाओं से विशिष्ट बनाता है, वह कहाँ था ? उसकी खोज कहाँ की जाती ? क्योंकि लड़कियों, जाँघों, दो अंगुल जगह, आत्म हत्याओं आदि के तनाव को कब तक घसीटा जा सकता था ? वह त्वरा जो कहानी की आंतरिक संगठना का मूल है, पहले घटनाओं से जीवित रहती थी। फिर चौंकानेवाले आकस्मिक झटकों में फँसी रही फिर यथार्थ वातावरण के सहारे जीवित रही। फिर प्रतीकों में उभरी संकेतों में भटकी और अभी परकता की तलाश तरह-तरह से की गई और इस प्रयास में कहानी अपने को तोड़ती रही और नये नये आयामों को जाँचती रही। और अब आकर कुछ एक कहानियों ने यह विश्वास दिया है कि कहानी को तोड़कर उसकी कहानीपरकता के पुराने प्रतिमानों को नकार कर, एक दूसरे स्तर पर कहानी को रूपायित किया जा सकता है, जहाँ किसी भी (दायित्व पूर्णता से चुने गये) कथ्य को कहानी का फ़ॉर्मा दिया जा सकता है, यानी उसकी कहानीपरकता (या विधागत विशिष्टता को) अक्षुण्ण रखा जा सकता है।
गंगाप्रसाद विमल, दूधनाथ सिंह, कामतानाथ, और कुछ हद तक पानू खोलिया की कहानियों में यह आंतरिक विशिष्टता देखी जा सकती है। ज्ञानरंजन की कहानियों में भी यह विशिष्टता थी। पर अब वह क्षीण हुई है। अवधनारायण सिंह की कहानियाँ भी इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं। अशोक सेकसरिया की दो तीन कहानियाँ इस बात की मिसाल हैं। इन लेखों ने बड़े दायित्व से कथ्यों के चुनाव किए हैं और कथात्मक लगने वाले संदर्भों को उठाकर ऐसा ढब दिया है कि कहानी-कहानी सी नहीं रह गई है। फिर भी वह कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। विधागत यह विशिष्टता उत्पन्न कर लेना एक बड़ी उपलब्धि है कि कहानी आपको कहानी न लगे और कहानी के अलावा वह और कुछ न हो। इन लेखकों की कुछ विशिष्ट ‘कहानियों’ के माध्यम से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है कि कहानीपन को काटकर इन्होंने कहानीपरकता को कहाँ से ग्रहण किया ? कामतानाथ की ‘छुट्टियाँ’, ‘दूधनाथ सिंह’, की ‘रीछ’ और अशोक सेकसरिया की ‘लेखकी’, गंगा प्रसाद विमल की ‘बीच की दरार’ कहानियों को उदाहरणस्वरूप लिया जा सकता है। पहली और मुख्य बात इनमें यही है कि इन्हें सिर्फ़ पढ़ा जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। यानी ये अनुभव का घनीभूत स्फुरण हैं। आत्मबोध की अभिव्यक्ति हैं। और कथात्मकता से परे हैं। (कथ्य की बात हम दूसरे संदर्भ में करेंगे) इन कहानियों के रेशों में, परिवेश में व्याप्त यातना और संताप का तनाव है। यह तनाव मात्र वैयक्तिक नहीं है, बल्कि समकालीन जीवन की टूटन और विसंगति की भयावह क्षुब्धता का प्रतिफलन है, कहानी की मंत्रणा आत्मिक होते हुए भी सामयिक से पृथक नहीं है।
यानी स्थितियों और परिवेश का तनाव और उसके मानसिक बिम्बों के रूपायन द्वारा कहानी एक और गति से चल सकती है। कहानीपरकता का यह मोड़ अब बीती कहानी का मोहताज नहीं है। इसने कथात्मकता और तन्मय गति का अपना स्रोत खोज लिया है।
इधर की कहानियों ने यह कहानीपरकता आत्मबोध और समयबोध के भीतर से ही प्राप्त की है...उनके संयमित संश्लेषण से। वह प्राथमिक रूप से बयान में, शब्दों में गुफन में नहीं है। बल्कि उस तनाव में है, जिसमें आज कहानी लिखी जा रही है। और तब कहानी के सभी अवयवों में वह व्याप्त हो जाती है।
और स्थूल रूप में कहें तो कथात्मकता का यह नया आयाम उस बोध से उपजा है जिसने आज की सक्रिय सर्जनशील प्रतिभा को पीस डालना चाहा है। यानी कहानी और लेखक के साक्षात्कार में कहीं परायापन नहीं है। कहानी ईमानदारी की हद तक ईमानदार है। जो उससे परे है, उसे वह अंगीकार नहीं करती। कहानीपरकता इतनी सेंसिटिव हो गई है कि अपने से बाहर के पदार्थ को वह मंजूर नहीं करती। यदि बाहर का पदार्थ उसमें प्रतिरोपित किया जाए तो या तो वह उस पदार्थ (या कथ्य) को मार देती है या स्वयं मर जाती है। जीवित कहानी का अहसास कहानीपरकता ही देती है। उसके इस नवीन व्यक्तित्व का अस्तित्व अब सामने है। यानी उसकी विशिष्ट और नयी कथात्मकता। कथात्मकता की जगह अब तनाव भरी कथ्यात्मकता ने ले ली है। यह एक महत्त्वपूर्ण संक्रमण है। कथ्य के कोण से देखने पर यह कहा जा सकता है कि कहानी पूर्ण स्वतंत्र हो गयी है, यानी कहानी ने कथ्य की वर्जनाओं को तोड़ दिया है।
कहानी अब किसी मतमतांतर राजनीतिक अवसरवादिता की अनुमतिचेता नहीं रही है। वह अब लेखक के प्रज्जवलित वक्तव्य की साक्षी है। यानी कहानी ने अपनी सत्ता की प्राप्ति कर ली है। कहानी में कहा गया तत्त्व औरों को कचोटता और संतप्त भी करता है। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि अन्य विधाओं के मुक़ाबले कहानी का कथ्य आज ज़्यादा व्यापक और सक्षम प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ज्वलंत संत्रास को आजकहानी ही ज़्यादा प्रखर रूप में पेश करती है। बौद्धिकता की चुनौती को बग़ैर अमूर्त हुए यह विद्या ही झेल सकती है। स्वयं अमूर्त को अभिव्यक्ति देने का दायित्व भी यह विद्या ही ज़्यादा प्रखर तथा डायरेक्ट हो गई है।
कहानियों का कथ्य भी इकहरा नहीं है। वह विषमता को समेटता है और कहानी एक बार में एक ही बात कह सकने की सीमा में आबद्ध नहीं है। कथ्य के साथ आघातों-संघातों का तनाव, आत्मबोध की आग और समयबोध का फैलाव भी रेशों में उठ-उठकर आता है।
चारों ओर व्याप्त संत्रास दंश, आक्रोश और विद्रोह को कहानी ने उठा लिया है। विसंगत और व्यर्थ को भी उठाकर अर्थ-सम्पन्न बना देने की कोशिश की है। जो कुछ नजर आता है, उससे तटस्थ होते हुए भी उसी से जूझने का संकल्प किया है। कहानियों का कथ्य अब बहुत गहरे में उतर गया है, जहाँ वह कभी-कभी दार्शनिकता की हदें भी छू लेती है। (अवधनारायण सिंह की ‘तीन घण्टे’, दूधनाथ सिंह की ‘रक्तपात’ काशीनाश सिंह की ‘आदमी का आदमी’, कामतानाथ की ‘छुट्टियाँ’, विमल की ‘बीच की दरार’, सुधा अरोड़ा की ‘आग’, मधुकर सिंह की ‘पूरा सन्नाटा’, अरविंद सक्सेना की ‘दुश्मनी’, हरवंश कश्यप की ‘तीसरा’ आदि कहानियाँ इस संदर्भ में देखी जा सकती हैं।)
कथ्य के स्तर पर जो परिवर्तन आया है, वह मूलतः चुनाव की (परंपरामुक्त और रुढ़िमुक्त) स्वतंत्रता का है। अब कहानी के कथ्य पर कोई हावी नहीं है। कहानीकारों ने राजनीतिक वादों (राजनीति से नहीं) परम्पराप्रेरित मंतव्यों घर-परिवारों की सीमाओं पतिपत्नी सम्बन्धों आदि के सतही और सहज कथाबिंदुओं से मुक्ति पा ली है। कहानी कहीं भी, किसी भी जगह कन्फ़ोर्मिन्ट नहीं रह गई है। वह अपने सिवा किसी भी सत्ता की ग़ुलाम नहीं है। न वह स्थापित मूल्यों की परवाह करती है और न मूल्यों की स्थापना को ज़रूरी मानती है। (रमेश उपाध्याय की ‘मछली’, और पानू खोलिया की ‘बरगद’, नरेन्द्र कोहली की ‘हिन्दुस्तानी’ संतोष की ‘अपमान’, कामतानाथ की ‘लाशें’, भीमसेन त्यागी की ‘महा नगर’, दूधनाथ सिंह की ‘रीछ’, अशोक सेकसरिया की ‘लेखकी’, अशोक आत्रेय की ‘मेरे पिता की विजय’ आदि कहानियाँ इस मुक्ति का प्रमाण हैं।)
कथ्य को लिरिकल स्वर पर उठाकर भीतर व्याप्त अकेलेपन के सन्नाटे और रोमांटिक व्यर्थता का अहसास करा देने की सहज क्षमता भी कुछ कहानियों में आयी है। प्रेमकथाओं से अलग विचित्र सी उदासी और ज़िन्दगी की बेहूदगी को प्रौढ़ स्वर में रूपायित करन का एक आयाम भी इधर उभरा है।
झीने प्यार की पीठिका में कुछ कहानियों ने दूसरा ही अनुभव देने की कोशिश की है। वह अनुभव है घुटन उदासी और अकेलेपन की टूटन का। पर घुटन उदासी की व्याप्ति केवल मन तक अटककर नहीं रह जाती। ऊपरी विषाद के नीचे व्यर्थता का बोध भी उभरता है, जो कि मात्र वैयक्तिक नहीं है, बल्कि उसकी जड़े अस्तित्व के सीमांत तक फैली हुई हैं। एक पावन उदासी ऊब, घुटन और शांत स्वीकृति का यह आयाम मृणाल पाण्डे एस.लाल. रवीन्द्र वर्मा, सांत्वना निगम देवकी अग्रवाल प्रकाश बाथम आदि की कहानियों में उभरा है।
कभी कभी कहानी का माहौल और उसकी घटनाएँ और उसके व्यक्ति बेहद परिचित होते हैं और उन्हें इस तरह पेश कर दिया जाता है जैसे वह मात्र सतही निरूपण हो। ऐसी कहानियाँ कभी-कभी बहुत खतरनाक साबित होती हैं, क्योंकि पहली बार में वे सिर्फ़ गुज़र जाती हैं, पुरानी तस्वीर की तरह। पर ज़रा गौर से पढ़ने पर ये मौन कहानियाँ इतना कुछ कहती हैं, जो साधारणतया एक कहानी में नहीं कहा जा सकता। निस्संग कला की ये मौन पर खतरनाक कहानियाँ अतिशय गहराई में से नियोजित हो पाती हैं। उन्हें सतह पर लाने के लिए बड़े सपाट तरीके़ से रख दिया जाता है। कामतानाथ की कई कहानियाँ इसी ख़तरनाक मौन अन्वेषण की कहानियाँ हैं। शरत् की कहानी जिसका शीर्षक शायद ‘दूसरा इतवार’ था और सुदीप की कहानी ‘यख़’ इस नवीन अन्वेषण में संलग्न हैं। वीरेंद्र दीपक की कहानी तफ़रीह इसी शैली में है। पर वे कथ्य का आभास देती चली है। और यह छूट नहीं देती कि पाठक कुछ अपना सोच सके। लेखक अपने पाठक को नज़रबंद कर लेता है। मौन कहानियों में उदासी का झीना आवरण भी है और एक अजीब क़िस्म की निस्संगता और मंथरता भी। पर ये कहानियाँ भीतर ही भीतर एक भीषण अंधड़ लिये उबलती रहती हैं। इनका कथ्य एक-एक शब्द में रिसता है। ये ख़ामोशी से एक गहन अनुभव देकर समाप्त हो जाती हैं। ‘छुट्टियाँ’ और ‘यख़’ ऐसी ही कहानियाँ हैं। ये तनाव पर नहीं जीतीं। ये कहानीकार की अनुभूति की प्रखरता पर टिकी हैं। और इनमें कहानी की आतंरिक संघटना पेण्टिग की तरह होती है। एक-एक रंग अपना अर्थ रखता है। एक-एक वाक्य और पैराग्राफ् सधा हुआ आता है।
इधर की कुछ कहानियाँ विस्फोट कही जा सकती हैं। ख़तरनाक ये भी हैं, पर मौन नहीं। इनमें लेखक की उपस्थिति के बग़ैर काम नहीं चलता। वह पात्र के रूप में हो या न हो, पर वह जिस जन्नाटे से शब्दों और वाक्यों में आता है, वह छुपा नहीं रहता। इन कथाओं में कुछ शब्द बार बार आते हैं, जो रचना के समय लेखक पर हावी हो जाते हैं। उन शब्दों की संगति कहानी के साथ भी निश्चय ही होती है। ऐसी कहानियाँ मूलतः अपने परिवेश के आक्रोश से संतप्त हैं और मुखर रूप से कुछ कहना ही चाहती हैं। दामोदर सदन, विश्वेश्वर माहेश्वर जितेंद्र भाटिया, अशोक आत्रेय और सिद्धेश की कुछ कहानियाँ लेखकीय आक्रोश और व्यक्तित्व की उपज हैं। मेहरुन्निसा परवेज की कथाओं में वह आक्रोश तो नहीं है, पर मुखरता का पक्ष विद्यमान हैं। कांता सिनहा की कहानियों में भी यह मुखरता है। पर वह कथात्मकता से कटी हुई नहीं है। माहेश्वर जितेंद्र सदन विश्वेश्वर सिद्धेश और आत्रेय को ‘बात’ कहनी होती है। यों चेतना के धरातल पर सदन, विश्वेश्वर और जितेंद्र भाटिया की कहानियाँ सबसे अलग हैं।
वल्लभ सिद्धार्थ और मंगलेश डबराल ने अपनी ही कुछ ही कहानियों से विशिष्ट आस्वाद दिया है। रंजीत कपूर की एक ही कहानी ‘नींद’ इस आस्वाद को और तीखा करती है। संयत बदहवासी और उसके माध्यम से किसी सत्य तक पहुँचने की आक्रोशभरी यात्रा बल्लभ सिद्धार्थ की कहानियों में है और अर्थ संदर्भों से भरी स्थितियाँ भी। इनकी कहानियाँ लेखकीय धीरज से सधी हुई हैं। यह विशेषता जितेंद्र भाटिया की कहानियों में भी है। खण्डित मानवीय संकल्पों, यातना और कष्ट के क्षुब्ध कर देने वाले स्वर तक पहुँचा देने की कथात्मक अन्विति विश्वेश्वर, जितेंद्र भाटिया, सुदीप और वल्लभ में विद्यमान है। वल्लभ की कहानियों का आवरण अनाकर्षक हो सकता है। पर उनके भीतर सीधे-सीधे आप यातना सहते हुए व्यक्तियों से मिल सकते हैं। जितेंद्र और अरविंद सक्सेना की कहानियों में आवरण आकर्षक है और उनके भीतर लेखक और पात्रों का सम्मिलित विक्षोभ है। मधुकर सिंह ने यही विक्षोभ व्यंग्य का तीखापन अख्तियार कर लेता है और अपरूप होकर आता है कि आप न लोगों को पहचान पाएँगे, न घटनाओं से एकात्मकता स्थापित कर पाएँगे,पर विक्षोभ से साक्षात्कार किए बगैर नहीं रह पाएँगे।
अशोक अग्रवाल की कहानियों में व्यंग्य का सूक्ष्म कलात्मक तनाव है। विभु कुमार में यह तनाव और भी प्रखर है और उनकी कहानियाँ विशिष्ट संदर्भों को उठाती हैं।
सभी नये और एकदम नये लेखकों की कहानियों में से गुज़रते हुए जिस दुनिया से सामना होता है, वह भयावह, विसंगत, विक्षुब्ध और सक्रिय है। लोग भीतर से बौखलाये और परेशान है। वे साधन सम्पन्न लोग नहीं हैं। अधिकांश व्यक्ति नौजवान हैं, जो यथास्थितिको मंजूर नहीं करते। व्यवस्था के प्रति वे क्रुद्ध हैं। उन्होंने इस दनिया को मंज़ूर नहीं किया है इसलिए सच्चाइयों का सामना करते हुए भी वे आगत के प्रति अनासक्त नहीं हैं। भविष्यवादी तो वे नहीं हैं, पर आगतवादी ज़रूर हैं। इधर का यह पूरा लेखन कोई सपना लेकर नहीं चल रहा है। क्योंकि निकट अतीत का इतिहास इतनी मूल्यहीनता अवसाद और विभ्रम से भरा हुआ है कि सपनों की रेखाएँ बन ही नहीं पायी हैं।
एक के बाद एक सपना टूटता गया है। अतः उन पर आस्था ही नहीं रह गई है। परन्तु जब वे एक दुनिया को नामंज़ूर करते हैं तो अपनी कुछ धारणाओं के कारण ही। वे धारणाएँ ही प्रमुख हैं, जो वर्तमान में उन्हें सक्रिय रखती हैं। ‘आग’ के रेंज अफ़सर की तरह हर व्यक्ति लहूलुहान और घायल है। संशयग्रस्त और विक्षुब्ध है। वह जंगल में चले जाने के पाखण्ड को भी जानता है। वह अपनी आत्मा, अपने कमज़ोरियों, इस दुनया की जघन्य बेहूदगियों और संत्रास से परिचित है-पर वह शून्य में नहीं है। बग़ैर सपनों के भी तो रातें कटती ही हैं-वह आगात की बात तो नहीं करता। पर जो नहीं आया है-उसका जवाब माँगता है। इन कहानियों की दुनिया आत्म-ग्लानि या पश्चात्ताप या संस्कारजन्य निरीहता की दुनिया तो नहीं ही है। यह फैशनपरस्तों की भी दुनिया नहीं है-यह दुनिया उन लोगों की है,जो इस दुनिया को अपने लिए चाहते हैं। अपनी तरह चाहते हैं। अपनी आकांक्षाओं के मातहत वर्तमान से विक्षुब्ध और कल के प्रति सचेत लोगों की दुनिया है। यह नौजबानों की दुनिया है और यह युवाशक्ति अपने संतुलनों, संबंधों और निष्कर्षों को लेकर जीना चाहती है ।
कहानी का सबसे बड़ा संकट ही यह होता कि वह आत्मबोध और समयबोध को किस स्तर पर स्वीकृत करे। कथात्मकता के स्तर पर या कथ्य के बिंदु पर या लेखक के अपने बोध के तनाव पर ?
अगर इस स्थिति को जरा और स्पष्ट करलिया जाए तो बात इकहरी हो जाने का खतरा है। पर विवेचन की सरलता के लिए इन आसंगों को अलग कर लिया जाना बेहतर है।
कथात्मकता का निर्वाह कर सकने के लिए रचना क्षणों में लेखकीय चेतना मूड़ों, स्थितियों, घटनाओं क्षणों मनःस्थितियों का संयमित चुनाव करती चलती है, ताकि कथ्य का यथार्थ खण्डित न होने पाए और वह अपने ‘फॉर्म’ की रक्षा भी कर ले जाए या कि कथ्य को एक ‘फॉर्म’ दे पाए। फॉर्म का यह झमेला बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि यह इतना दबाव डालता है कि कभी-कभी कहानी वह नहीं बन पाती, जो उसकी नियति थी। कुछ लेखकों के लिए कथात्मकता नैरेटिव या स्ट्रक्चर का पर्याय है, कि कहानी का रूपबंध क्या है, कि उसकी विकास सरणी क्या है। सर्जनात्मक प्रतिभा के लिए यह बाहरी उपादन व्यर्थ होते हैं। सर्जनात्मक प्रतिभा अपनी कथात्मकता के लिए दूसरे दर्जे के यथार्थवादी वातावरण या तथ्यसम्मत सम्भावनाओं के व्यामोह में नहीं पड़ती। वह फ़ॉर्म की तलाश भी नहीं करती और न अपनी घटित स्थितियों के बयान के लिए होटलों नाचघरों या बिस्तरों के कोने खोजती है। बहुत दिनों तक फ़ॉर्म की रक्षा (एक तरह से) कहानी में लड़की की उपस्थिति करती रही। अगर कहानी में लड़की न होती तो मूड्स के टुकड़े जुड़ नहीं पाते, लड़की के बाद यह काम स्त्री की जाँघों से लिया जाने लगा।
और फिर, दो अंगुल जगह से। कुछ कोशिश आत्महत्या के तनाव को इस्तेमाल करके की गई। कभी-कभी मात्र सैक्स चित्रण के सहारे कहानी की गति को बरकरार रखा गया; और जहाँ वह सब नहीं मिला, वहीं कहानी पहले ही पैराग्राफ़ पर घुटने तोड़कर बैठ गई। यानी कहानी पढ़ी नहीं गई। पिछले दिनों का छपित साहित्य इसका प्रमाण है कि चीजें छपीं, पर पढ़ी नहीं गईं। साहित्यनिष्ठ लोग जैसे तैसे पढ़ते भी रहे, पर उनके मानस पर कुछ घटित नहीं हुआ। हुआ यह कि कथात्मकता की सार्थक भंगिमा को नये धरातल पर बहुतों ने आत्मसात नहीं कर पाया, अपने समय के दबाव-तनाव और विक्रिया को नहीं समझा। बहुतों को यही लगा कि कुछ भी बक दिया जाय, वह कहानी हो जायेगी। कहानी की ऊपरी सहजता ने एक मृगछलना का काम किया और कहानीकार हो सकने की प्यास में उस मृगछलना के पीछे दौड़ते-दौड़ते बहुत से बेहोश होकर गिर पड़े। बहुतों ने दम तोड़ दिया।
सवाल था कि कहानी की यह कहानीपरकता थी भी कहाँ ? यानी कहानी का अपना वह फॉर्म जो उसे अन्य विधाओं से विशिष्ट बनाता है, वह कहाँ था ? उसकी खोज कहाँ की जाती ? क्योंकि लड़कियों, जाँघों, दो अंगुल जगह, आत्म हत्याओं आदि के तनाव को कब तक घसीटा जा सकता था ? वह त्वरा जो कहानी की आंतरिक संगठना का मूल है, पहले घटनाओं से जीवित रहती थी। फिर चौंकानेवाले आकस्मिक झटकों में फँसी रही फिर यथार्थ वातावरण के सहारे जीवित रही। फिर प्रतीकों में उभरी संकेतों में भटकी और अभी परकता की तलाश तरह-तरह से की गई और इस प्रयास में कहानी अपने को तोड़ती रही और नये नये आयामों को जाँचती रही। और अब आकर कुछ एक कहानियों ने यह विश्वास दिया है कि कहानी को तोड़कर उसकी कहानीपरकता के पुराने प्रतिमानों को नकार कर, एक दूसरे स्तर पर कहानी को रूपायित किया जा सकता है, जहाँ किसी भी (दायित्व पूर्णता से चुने गये) कथ्य को कहानी का फ़ॉर्मा दिया जा सकता है, यानी उसकी कहानीपरकता (या विधागत विशिष्टता को) अक्षुण्ण रखा जा सकता है।
गंगाप्रसाद विमल, दूधनाथ सिंह, कामतानाथ, और कुछ हद तक पानू खोलिया की कहानियों में यह आंतरिक विशिष्टता देखी जा सकती है। ज्ञानरंजन की कहानियों में भी यह विशिष्टता थी। पर अब वह क्षीण हुई है। अवधनारायण सिंह की कहानियाँ भी इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं। अशोक सेकसरिया की दो तीन कहानियाँ इस बात की मिसाल हैं। इन लेखों ने बड़े दायित्व से कथ्यों के चुनाव किए हैं और कथात्मक लगने वाले संदर्भों को उठाकर ऐसा ढब दिया है कि कहानी-कहानी सी नहीं रह गई है। फिर भी वह कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। विधागत यह विशिष्टता उत्पन्न कर लेना एक बड़ी उपलब्धि है कि कहानी आपको कहानी न लगे और कहानी के अलावा वह और कुछ न हो। इन लेखकों की कुछ विशिष्ट ‘कहानियों’ के माध्यम से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है कि कहानीपन को काटकर इन्होंने कहानीपरकता को कहाँ से ग्रहण किया ? कामतानाथ की ‘छुट्टियाँ’, ‘दूधनाथ सिंह’, की ‘रीछ’ और अशोक सेकसरिया की ‘लेखकी’, गंगा प्रसाद विमल की ‘बीच की दरार’ कहानियों को उदाहरणस्वरूप लिया जा सकता है। पहली और मुख्य बात इनमें यही है कि इन्हें सिर्फ़ पढ़ा जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। यानी ये अनुभव का घनीभूत स्फुरण हैं। आत्मबोध की अभिव्यक्ति हैं। और कथात्मकता से परे हैं। (कथ्य की बात हम दूसरे संदर्भ में करेंगे) इन कहानियों के रेशों में, परिवेश में व्याप्त यातना और संताप का तनाव है। यह तनाव मात्र वैयक्तिक नहीं है, बल्कि समकालीन जीवन की टूटन और विसंगति की भयावह क्षुब्धता का प्रतिफलन है, कहानी की मंत्रणा आत्मिक होते हुए भी सामयिक से पृथक नहीं है।
यानी स्थितियों और परिवेश का तनाव और उसके मानसिक बिम्बों के रूपायन द्वारा कहानी एक और गति से चल सकती है। कहानीपरकता का यह मोड़ अब बीती कहानी का मोहताज नहीं है। इसने कथात्मकता और तन्मय गति का अपना स्रोत खोज लिया है।
इधर की कहानियों ने यह कहानीपरकता आत्मबोध और समयबोध के भीतर से ही प्राप्त की है...उनके संयमित संश्लेषण से। वह प्राथमिक रूप से बयान में, शब्दों में गुफन में नहीं है। बल्कि उस तनाव में है, जिसमें आज कहानी लिखी जा रही है। और तब कहानी के सभी अवयवों में वह व्याप्त हो जाती है।
और स्थूल रूप में कहें तो कथात्मकता का यह नया आयाम उस बोध से उपजा है जिसने आज की सक्रिय सर्जनशील प्रतिभा को पीस डालना चाहा है। यानी कहानी और लेखक के साक्षात्कार में कहीं परायापन नहीं है। कहानी ईमानदारी की हद तक ईमानदार है। जो उससे परे है, उसे वह अंगीकार नहीं करती। कहानीपरकता इतनी सेंसिटिव हो गई है कि अपने से बाहर के पदार्थ को वह मंजूर नहीं करती। यदि बाहर का पदार्थ उसमें प्रतिरोपित किया जाए तो या तो वह उस पदार्थ (या कथ्य) को मार देती है या स्वयं मर जाती है। जीवित कहानी का अहसास कहानीपरकता ही देती है। उसके इस नवीन व्यक्तित्व का अस्तित्व अब सामने है। यानी उसकी विशिष्ट और नयी कथात्मकता। कथात्मकता की जगह अब तनाव भरी कथ्यात्मकता ने ले ली है। यह एक महत्त्वपूर्ण संक्रमण है। कथ्य के कोण से देखने पर यह कहा जा सकता है कि कहानी पूर्ण स्वतंत्र हो गयी है, यानी कहानी ने कथ्य की वर्जनाओं को तोड़ दिया है।
कहानी अब किसी मतमतांतर राजनीतिक अवसरवादिता की अनुमतिचेता नहीं रही है। वह अब लेखक के प्रज्जवलित वक्तव्य की साक्षी है। यानी कहानी ने अपनी सत्ता की प्राप्ति कर ली है। कहानी में कहा गया तत्त्व औरों को कचोटता और संतप्त भी करता है। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि अन्य विधाओं के मुक़ाबले कहानी का कथ्य आज ज़्यादा व्यापक और सक्षम प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ज्वलंत संत्रास को आजकहानी ही ज़्यादा प्रखर रूप में पेश करती है। बौद्धिकता की चुनौती को बग़ैर अमूर्त हुए यह विद्या ही झेल सकती है। स्वयं अमूर्त को अभिव्यक्ति देने का दायित्व भी यह विद्या ही ज़्यादा प्रखर तथा डायरेक्ट हो गई है।
कहानियों का कथ्य भी इकहरा नहीं है। वह विषमता को समेटता है और कहानी एक बार में एक ही बात कह सकने की सीमा में आबद्ध नहीं है। कथ्य के साथ आघातों-संघातों का तनाव, आत्मबोध की आग और समयबोध का फैलाव भी रेशों में उठ-उठकर आता है।
चारों ओर व्याप्त संत्रास दंश, आक्रोश और विद्रोह को कहानी ने उठा लिया है। विसंगत और व्यर्थ को भी उठाकर अर्थ-सम्पन्न बना देने की कोशिश की है। जो कुछ नजर आता है, उससे तटस्थ होते हुए भी उसी से जूझने का संकल्प किया है। कहानियों का कथ्य अब बहुत गहरे में उतर गया है, जहाँ वह कभी-कभी दार्शनिकता की हदें भी छू लेती है। (अवधनारायण सिंह की ‘तीन घण्टे’, दूधनाथ सिंह की ‘रक्तपात’ काशीनाश सिंह की ‘आदमी का आदमी’, कामतानाथ की ‘छुट्टियाँ’, विमल की ‘बीच की दरार’, सुधा अरोड़ा की ‘आग’, मधुकर सिंह की ‘पूरा सन्नाटा’, अरविंद सक्सेना की ‘दुश्मनी’, हरवंश कश्यप की ‘तीसरा’ आदि कहानियाँ इस संदर्भ में देखी जा सकती हैं।)
कथ्य के स्तर पर जो परिवर्तन आया है, वह मूलतः चुनाव की (परंपरामुक्त और रुढ़िमुक्त) स्वतंत्रता का है। अब कहानी के कथ्य पर कोई हावी नहीं है। कहानीकारों ने राजनीतिक वादों (राजनीति से नहीं) परम्पराप्रेरित मंतव्यों घर-परिवारों की सीमाओं पतिपत्नी सम्बन्धों आदि के सतही और सहज कथाबिंदुओं से मुक्ति पा ली है। कहानी कहीं भी, किसी भी जगह कन्फ़ोर्मिन्ट नहीं रह गई है। वह अपने सिवा किसी भी सत्ता की ग़ुलाम नहीं है। न वह स्थापित मूल्यों की परवाह करती है और न मूल्यों की स्थापना को ज़रूरी मानती है। (रमेश उपाध्याय की ‘मछली’, और पानू खोलिया की ‘बरगद’, नरेन्द्र कोहली की ‘हिन्दुस्तानी’ संतोष की ‘अपमान’, कामतानाथ की ‘लाशें’, भीमसेन त्यागी की ‘महा नगर’, दूधनाथ सिंह की ‘रीछ’, अशोक सेकसरिया की ‘लेखकी’, अशोक आत्रेय की ‘मेरे पिता की विजय’ आदि कहानियाँ इस मुक्ति का प्रमाण हैं।)
कथ्य को लिरिकल स्वर पर उठाकर भीतर व्याप्त अकेलेपन के सन्नाटे और रोमांटिक व्यर्थता का अहसास करा देने की सहज क्षमता भी कुछ कहानियों में आयी है। प्रेमकथाओं से अलग विचित्र सी उदासी और ज़िन्दगी की बेहूदगी को प्रौढ़ स्वर में रूपायित करन का एक आयाम भी इधर उभरा है।
झीने प्यार की पीठिका में कुछ कहानियों ने दूसरा ही अनुभव देने की कोशिश की है। वह अनुभव है घुटन उदासी और अकेलेपन की टूटन का। पर घुटन उदासी की व्याप्ति केवल मन तक अटककर नहीं रह जाती। ऊपरी विषाद के नीचे व्यर्थता का बोध भी उभरता है, जो कि मात्र वैयक्तिक नहीं है, बल्कि उसकी जड़े अस्तित्व के सीमांत तक फैली हुई हैं। एक पावन उदासी ऊब, घुटन और शांत स्वीकृति का यह आयाम मृणाल पाण्डे एस.लाल. रवीन्द्र वर्मा, सांत्वना निगम देवकी अग्रवाल प्रकाश बाथम आदि की कहानियों में उभरा है।
कभी कभी कहानी का माहौल और उसकी घटनाएँ और उसके व्यक्ति बेहद परिचित होते हैं और उन्हें इस तरह पेश कर दिया जाता है जैसे वह मात्र सतही निरूपण हो। ऐसी कहानियाँ कभी-कभी बहुत खतरनाक साबित होती हैं, क्योंकि पहली बार में वे सिर्फ़ गुज़र जाती हैं, पुरानी तस्वीर की तरह। पर ज़रा गौर से पढ़ने पर ये मौन कहानियाँ इतना कुछ कहती हैं, जो साधारणतया एक कहानी में नहीं कहा जा सकता। निस्संग कला की ये मौन पर खतरनाक कहानियाँ अतिशय गहराई में से नियोजित हो पाती हैं। उन्हें सतह पर लाने के लिए बड़े सपाट तरीके़ से रख दिया जाता है। कामतानाथ की कई कहानियाँ इसी ख़तरनाक मौन अन्वेषण की कहानियाँ हैं। शरत् की कहानी जिसका शीर्षक शायद ‘दूसरा इतवार’ था और सुदीप की कहानी ‘यख़’ इस नवीन अन्वेषण में संलग्न हैं। वीरेंद्र दीपक की कहानी तफ़रीह इसी शैली में है। पर वे कथ्य का आभास देती चली है। और यह छूट नहीं देती कि पाठक कुछ अपना सोच सके। लेखक अपने पाठक को नज़रबंद कर लेता है। मौन कहानियों में उदासी का झीना आवरण भी है और एक अजीब क़िस्म की निस्संगता और मंथरता भी। पर ये कहानियाँ भीतर ही भीतर एक भीषण अंधड़ लिये उबलती रहती हैं। इनका कथ्य एक-एक शब्द में रिसता है। ये ख़ामोशी से एक गहन अनुभव देकर समाप्त हो जाती हैं। ‘छुट्टियाँ’ और ‘यख़’ ऐसी ही कहानियाँ हैं। ये तनाव पर नहीं जीतीं। ये कहानीकार की अनुभूति की प्रखरता पर टिकी हैं। और इनमें कहानी की आतंरिक संघटना पेण्टिग की तरह होती है। एक-एक रंग अपना अर्थ रखता है। एक-एक वाक्य और पैराग्राफ् सधा हुआ आता है।
इधर की कुछ कहानियाँ विस्फोट कही जा सकती हैं। ख़तरनाक ये भी हैं, पर मौन नहीं। इनमें लेखक की उपस्थिति के बग़ैर काम नहीं चलता। वह पात्र के रूप में हो या न हो, पर वह जिस जन्नाटे से शब्दों और वाक्यों में आता है, वह छुपा नहीं रहता। इन कथाओं में कुछ शब्द बार बार आते हैं, जो रचना के समय लेखक पर हावी हो जाते हैं। उन शब्दों की संगति कहानी के साथ भी निश्चय ही होती है। ऐसी कहानियाँ मूलतः अपने परिवेश के आक्रोश से संतप्त हैं और मुखर रूप से कुछ कहना ही चाहती हैं। दामोदर सदन, विश्वेश्वर माहेश्वर जितेंद्र भाटिया, अशोक आत्रेय और सिद्धेश की कुछ कहानियाँ लेखकीय आक्रोश और व्यक्तित्व की उपज हैं। मेहरुन्निसा परवेज की कथाओं में वह आक्रोश तो नहीं है, पर मुखरता का पक्ष विद्यमान हैं। कांता सिनहा की कहानियों में भी यह मुखरता है। पर वह कथात्मकता से कटी हुई नहीं है। माहेश्वर जितेंद्र सदन विश्वेश्वर सिद्धेश और आत्रेय को ‘बात’ कहनी होती है। यों चेतना के धरातल पर सदन, विश्वेश्वर और जितेंद्र भाटिया की कहानियाँ सबसे अलग हैं।
वल्लभ सिद्धार्थ और मंगलेश डबराल ने अपनी ही कुछ ही कहानियों से विशिष्ट आस्वाद दिया है। रंजीत कपूर की एक ही कहानी ‘नींद’ इस आस्वाद को और तीखा करती है। संयत बदहवासी और उसके माध्यम से किसी सत्य तक पहुँचने की आक्रोशभरी यात्रा बल्लभ सिद्धार्थ की कहानियों में है और अर्थ संदर्भों से भरी स्थितियाँ भी। इनकी कहानियाँ लेखकीय धीरज से सधी हुई हैं। यह विशेषता जितेंद्र भाटिया की कहानियों में भी है। खण्डित मानवीय संकल्पों, यातना और कष्ट के क्षुब्ध कर देने वाले स्वर तक पहुँचा देने की कथात्मक अन्विति विश्वेश्वर, जितेंद्र भाटिया, सुदीप और वल्लभ में विद्यमान है। वल्लभ की कहानियों का आवरण अनाकर्षक हो सकता है। पर उनके भीतर सीधे-सीधे आप यातना सहते हुए व्यक्तियों से मिल सकते हैं। जितेंद्र और अरविंद सक्सेना की कहानियों में आवरण आकर्षक है और उनके भीतर लेखक और पात्रों का सम्मिलित विक्षोभ है। मधुकर सिंह ने यही विक्षोभ व्यंग्य का तीखापन अख्तियार कर लेता है और अपरूप होकर आता है कि आप न लोगों को पहचान पाएँगे, न घटनाओं से एकात्मकता स्थापित कर पाएँगे,पर विक्षोभ से साक्षात्कार किए बगैर नहीं रह पाएँगे।
अशोक अग्रवाल की कहानियों में व्यंग्य का सूक्ष्म कलात्मक तनाव है। विभु कुमार में यह तनाव और भी प्रखर है और उनकी कहानियाँ विशिष्ट संदर्भों को उठाती हैं।
सभी नये और एकदम नये लेखकों की कहानियों में से गुज़रते हुए जिस दुनिया से सामना होता है, वह भयावह, विसंगत, विक्षुब्ध और सक्रिय है। लोग भीतर से बौखलाये और परेशान है। वे साधन सम्पन्न लोग नहीं हैं। अधिकांश व्यक्ति नौजवान हैं, जो यथास्थितिको मंजूर नहीं करते। व्यवस्था के प्रति वे क्रुद्ध हैं। उन्होंने इस दनिया को मंज़ूर नहीं किया है इसलिए सच्चाइयों का सामना करते हुए भी वे आगत के प्रति अनासक्त नहीं हैं। भविष्यवादी तो वे नहीं हैं, पर आगतवादी ज़रूर हैं। इधर का यह पूरा लेखन कोई सपना लेकर नहीं चल रहा है। क्योंकि निकट अतीत का इतिहास इतनी मूल्यहीनता अवसाद और विभ्रम से भरा हुआ है कि सपनों की रेखाएँ बन ही नहीं पायी हैं।
एक के बाद एक सपना टूटता गया है। अतः उन पर आस्था ही नहीं रह गई है। परन्तु जब वे एक दुनिया को नामंज़ूर करते हैं तो अपनी कुछ धारणाओं के कारण ही। वे धारणाएँ ही प्रमुख हैं, जो वर्तमान में उन्हें सक्रिय रखती हैं। ‘आग’ के रेंज अफ़सर की तरह हर व्यक्ति लहूलुहान और घायल है। संशयग्रस्त और विक्षुब्ध है। वह जंगल में चले जाने के पाखण्ड को भी जानता है। वह अपनी आत्मा, अपने कमज़ोरियों, इस दुनया की जघन्य बेहूदगियों और संत्रास से परिचित है-पर वह शून्य में नहीं है। बग़ैर सपनों के भी तो रातें कटती ही हैं-वह आगात की बात तो नहीं करता। पर जो नहीं आया है-उसका जवाब माँगता है। इन कहानियों की दुनिया आत्म-ग्लानि या पश्चात्ताप या संस्कारजन्य निरीहता की दुनिया तो नहीं ही है। यह फैशनपरस्तों की भी दुनिया नहीं है-यह दुनिया उन लोगों की है,जो इस दुनिया को अपने लिए चाहते हैं। अपनी तरह चाहते हैं। अपनी आकांक्षाओं के मातहत वर्तमान से विक्षुब्ध और कल के प्रति सचेत लोगों की दुनिया है। यह नौजबानों की दुनिया है और यह युवाशक्ति अपने संतुलनों, संबंधों और निष्कर्षों को लेकर जीना चाहती है ।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i