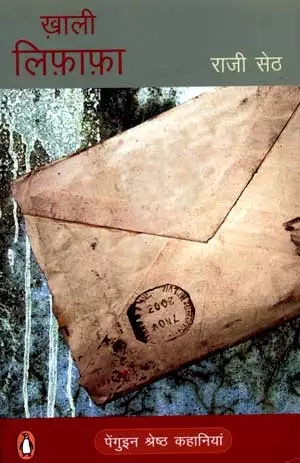|
कहानी संग्रह >> अन्धे मोड़ से आगे अन्धे मोड़ से आगेराजी सेठ
|
101 पाठक हैं |
|||||||
मानवीय संबंधों के द्वन्द्व और अन्तर्द्वन्द्व की कुछ कहानियाँ
Andehere Mod se Aage a hindi book by Raji Seth - अन्धे मोड़ से आगे - राजी सेठ
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मानवीय संबंधों के द्वन्द्व और अन्तर्द्वन्द्व की आन्तरिक विकलता, मंथर प्रवाह और गहराई; कथ्य-चयन में संकेन्द्रण, शिल्प रचने का धीरज, कृति की सधी हुई कोठी-बेहद कमसिन, लचीली मगर भीतर से मजबूत इरादे की तरह राजी की विशेषताएँ हैं। ऐसे रचना गुण कुछ अलग संयोजनों में या अन्य लेखकों में भी कमोबेश मिल जाएँगे परन्तु इन्हें एक अलग स्पर्श और लावण्य देती है राजी की ‘स्त्री’ जो वहाँ सिर्फ संवेदना में ही नहीं, जैविक पदार्थता में भी है। पुरुष-स्पर्द्धी आधुनिक स्त्री की तरह राजी अपने लेखन में न तो स्त्री होने से इनकार करती हैं और न उसे नष्ट करती हैं, बल्कि अपने नैसर्गित रुप में उसकी शक्ति और सम्भावना, उसके सत्य और अनुभव, उसकी नियति और उत्कटता का वह सृजनात्मक उपयोग करती हैं। स्त्री होने को स्वीकारते हुए, राजी के लेखक ने इस स्वीकार के भीतर जितने इनकार रचे हैं, यथास्थिति में जितने हस्तक्षेप किए हैं, उसे उनकी आधुनिकत पहचान के लिए देखना जरुरी है। राजी ने स्त्री के भीतर पराजित पुरुष को; बल्कि व्यवस्था को, जितनी भंगिमाओं में उकेरा है और अपनी विंध्यात्मक दृष्टि से जो मूल्यवत्ता अर्जित की है, उससे नए-नए सृष्ट्यर्थ प्रकट हुए हैं। वे ऐसी महिलावादी नहीं है जिन्हें पुरुष नकरात्मक उपस्थिति लगता है, वे स्त्री की खोट भी पहचानने की कोशिश करती हैं और भरसक निरपेक्ष बनी रहकर अधिक विश्वासनीय होती हैं। वे बार-बार इस प्रश्न से जूझती हैं कि क्या समाज आधुनिकता के नाम पर जारी विघटनों के विद्रूपों के सहारे जिन्दा रह सकेगा। अपने को देखता हुआ लेखक इसका साभिप्राय और सचेष्ट उपयोग कर सके तो वह व्यक्तित्व को विशिष्टता देता है और रचना को विरलता। राजी इसी वास्ते धारा में भी अलग हैं। अपनी पहचान आप। राजी की कहानियाँ हिन्दी जगत में एक अलग जगह की अधिकारी हैं और अलग ढंग से बात करने की जरुरत महसूस कराती हैं।
अन्धे मोड़ से आगे
यह संकलन....
अपने प्रथम प्रयास के रूप में इस कहानी-संकलन को आपके हाथों में देते हुए मुझे एक संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर वह सब है—जो आज तक मैंने पढ़ा या जाना, जो मुझे छेदता, भेदता, कोंचता, छूता रहा ; संवेदनों की तराश और परिष्कार के रूप में मेरे बोधों को रूपान्तरित करता एक दृष्टि के रूप में मुझे उपलब्ध हुआ ; उस सारे के सारे चेत, तराश, ज्ञान और दृष्टि का एक मूल्य-सजग बोध और दूसरी ओर मैं...एक अकेली, अनगढ़ मैं और इन कहानियों के रूप में चित्रित मेरी मानसिकता और संवेदना।
यह चेत मुझे इस क्षण पूरा है कि मैं चाहे लेखक हूँ या नहीं भी, एक सचेत पाठक अवश्य रही क्योंकि साहित्य से मेरा नाता कर्म का नहीं, निष्ठा का रहा। साहित्य में, जितने कुछ को मैंने एक पाठकीय अधिकार से स्वीकार किया या उसी अधिकार से नकारा भी, एक लेखक की हैसियत से मुझमें उन मर्यादाओं का अतिक्रमण करने की क्षमता, अपने को उतना ही साफ देख सकने का निष्पक्ष साहस और पाठकों की रचनात्मक अपेक्षाएँ पूरी करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, नहीं तो एक पाठक के रूप में लेखक से मेरी किन्हीं अपेक्षाओं का कोई औचित्य नहीं। लेखक-रूप में अपनी इसी मर्यादा का अहसास—दर्दीला एहसास—इस समय मेरे मन में है, और उत्तरदायित्व के पूरे वजन के साथ है।
‘अच्छी कहानी’ क्या होती है, इसका ज्ञान ही मेरे मन में अपनी इस मर्यादा की पहचान पैदा कर रहा है, चाहे वह कितना भी यातनामय क्यों न हो। मुझे स्वीकारना होगा कि अच्छी कहानी इतनी, ऐसी या यही नहीं है, वह इससे अधिक सुघड़, जीवन्त, अधिक दृष्टि-सम्पन्न, इससे आगे और अधिक सम्पूर्ण होती है। सम्पूर्णता को यदि मिथ भी मान लें तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि यात्रा में जो कदम वज़नदार पड़ते हैं वे ही अपने निशान छोड़ते हैं।
अतः ‘अच्छी’ कहानी और ‘मेरी’ कहानी के बीच जितना फासला है, उसका एहसास मुझे पूरा है और इसका भी कि लेखन में किसी स्तर तक पहुँचने का रास्ता मात्र लेखन से ही पाटना होता है, उसका कोई शार्टकट नहीं होता। लिखना, लिखते रहना ही लेखन के आन्तरिक सत्व और विवेक को पा सकने का साधन है। यह वह जगत है जहाँ तरणी और तट, साधन और साध्य एकरूप हैं, शायद इसीलिए यात्रारम्भ और गन्तव्य के बीच मिली थकान और तपन, व्यर्थता और अपूर्णता सह्य हो जाती है। हताश नहीं होने देती, लिखते रहने की आस्था को भीतर कहीं जागृत रखती है।
मैं यात्रा में हूँ, बल्कि यात्रारम्भ पर, इसे स्वीकारने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मेरी ये कहानियाँ मेरी संवेदना के स्नैपशॉट्स हैं, कैमरे के निमिष पल को खुलती आँख में बन्दी क्षण। अपनी सम्पूर्ण आन्तरिक चेतन-सृष्टि की अर्थ-चौंध में जो, जितना, जैसा भी पकड़ में आया—वह वैसा क्षण। उस पकड़ में बहुत कुछ छूट गया भी हो सकता है, परन्तु वही तो मेरे यात्रा में होने की पहचान है। जितना मेरी पकड़ में है, सत्य उतना ही नहीं है, परन्तु सत्य के इतने मात्र को मैं छू पाई हूँ, मेरी इतनी सच्चाई है।
मेरा लेखकीय जीवन अत्यन्त संक्षिप्त है—मात्र तीन वर्ष का, परन्तु यह कहना समुचित न होगा कि बोधों की आयु भी इतनी है। लेखन में सक्रियता के क्षण मात्र उन्हें बाँधने के क्षण हैं, ऊर्जा तो बोध-जगत की ही होती है। इस बोध-यात्रा में जितना कुछ भी-व्यक्ति, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ—मेरे साथ रहा है और मेरे अस्ति-बिन्दु को संवेदना-विस्तार द्वारा परिधि देता रहा है, उन सबके प्रति मेरा आन्तरिक आभार। उन सबने ही मुझे यह क्षण दिया है, पहले अपना फिर आप सबका सामना कर सकने का।
यह चेत मुझे इस क्षण पूरा है कि मैं चाहे लेखक हूँ या नहीं भी, एक सचेत पाठक अवश्य रही क्योंकि साहित्य से मेरा नाता कर्म का नहीं, निष्ठा का रहा। साहित्य में, जितने कुछ को मैंने एक पाठकीय अधिकार से स्वीकार किया या उसी अधिकार से नकारा भी, एक लेखक की हैसियत से मुझमें उन मर्यादाओं का अतिक्रमण करने की क्षमता, अपने को उतना ही साफ देख सकने का निष्पक्ष साहस और पाठकों की रचनात्मक अपेक्षाएँ पूरी करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, नहीं तो एक पाठक के रूप में लेखक से मेरी किन्हीं अपेक्षाओं का कोई औचित्य नहीं। लेखक-रूप में अपनी इसी मर्यादा का अहसास—दर्दीला एहसास—इस समय मेरे मन में है, और उत्तरदायित्व के पूरे वजन के साथ है।
‘अच्छी कहानी’ क्या होती है, इसका ज्ञान ही मेरे मन में अपनी इस मर्यादा की पहचान पैदा कर रहा है, चाहे वह कितना भी यातनामय क्यों न हो। मुझे स्वीकारना होगा कि अच्छी कहानी इतनी, ऐसी या यही नहीं है, वह इससे अधिक सुघड़, जीवन्त, अधिक दृष्टि-सम्पन्न, इससे आगे और अधिक सम्पूर्ण होती है। सम्पूर्णता को यदि मिथ भी मान लें तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि यात्रा में जो कदम वज़नदार पड़ते हैं वे ही अपने निशान छोड़ते हैं।
अतः ‘अच्छी’ कहानी और ‘मेरी’ कहानी के बीच जितना फासला है, उसका एहसास मुझे पूरा है और इसका भी कि लेखन में किसी स्तर तक पहुँचने का रास्ता मात्र लेखन से ही पाटना होता है, उसका कोई शार्टकट नहीं होता। लिखना, लिखते रहना ही लेखन के आन्तरिक सत्व और विवेक को पा सकने का साधन है। यह वह जगत है जहाँ तरणी और तट, साधन और साध्य एकरूप हैं, शायद इसीलिए यात्रारम्भ और गन्तव्य के बीच मिली थकान और तपन, व्यर्थता और अपूर्णता सह्य हो जाती है। हताश नहीं होने देती, लिखते रहने की आस्था को भीतर कहीं जागृत रखती है।
मैं यात्रा में हूँ, बल्कि यात्रारम्भ पर, इसे स्वीकारने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मेरी ये कहानियाँ मेरी संवेदना के स्नैपशॉट्स हैं, कैमरे के निमिष पल को खुलती आँख में बन्दी क्षण। अपनी सम्पूर्ण आन्तरिक चेतन-सृष्टि की अर्थ-चौंध में जो, जितना, जैसा भी पकड़ में आया—वह वैसा क्षण। उस पकड़ में बहुत कुछ छूट गया भी हो सकता है, परन्तु वही तो मेरे यात्रा में होने की पहचान है। जितना मेरी पकड़ में है, सत्य उतना ही नहीं है, परन्तु सत्य के इतने मात्र को मैं छू पाई हूँ, मेरी इतनी सच्चाई है।
मेरा लेखकीय जीवन अत्यन्त संक्षिप्त है—मात्र तीन वर्ष का, परन्तु यह कहना समुचित न होगा कि बोधों की आयु भी इतनी है। लेखन में सक्रियता के क्षण मात्र उन्हें बाँधने के क्षण हैं, ऊर्जा तो बोध-जगत की ही होती है। इस बोध-यात्रा में जितना कुछ भी-व्यक्ति, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ—मेरे साथ रहा है और मेरे अस्ति-बिन्दु को संवेदना-विस्तार द्वारा परिधि देता रहा है, उन सबके प्रति मेरा आन्तरिक आभार। उन सबने ही मुझे यह क्षण दिया है, पहले अपना फिर आप सबका सामना कर सकने का।
दूसरे संस्करण की भूमिका
प्रथम पुस्तक की आवृत्ति मेरे लिए एक सुखद संयोग है। पहला संस्करण 1979 में राजपाल एंड सन्ज़ से छपा था।
एकाध कहानी में अनुच्छेदों के मूल क्रम में तथा अन्य कहानियों में शाब्दिक हेर-फेर हुए हैं। कहना न होगा कि इन वर्षों में भारत के साथ निरन्तर बदलते रिश्ते का एहसास बराबर बना रहा है। यह अहसास सायास से निरायास, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, साथ ही वर्णित में से निहित अर्थ में और अधिक खुल सकने और सम्प्रेषित हो सकने की जीवन्त बेचैनी में मुझे सदा अवस्थित रखता रहा है।
जहाँ तक कथ्य का प्रश्न है, वह वैसे का वैसा है—उस कालखंड में जीवन के निरीक्षण-परीक्षण की निजी तत्कालिक पहचान दे सकने के कारण—अस्पर्श। उसे छेड़ सकने का अधिकार लेखक का कहाँ रहता है !
एकाध कहानी में अनुच्छेदों के मूल क्रम में तथा अन्य कहानियों में शाब्दिक हेर-फेर हुए हैं। कहना न होगा कि इन वर्षों में भारत के साथ निरन्तर बदलते रिश्ते का एहसास बराबर बना रहा है। यह अहसास सायास से निरायास, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, साथ ही वर्णित में से निहित अर्थ में और अधिक खुल सकने और सम्प्रेषित हो सकने की जीवन्त बेचैनी में मुझे सदा अवस्थित रखता रहा है।
जहाँ तक कथ्य का प्रश्न है, वह वैसे का वैसा है—उस कालखंड में जीवन के निरीक्षण-परीक्षण की निजी तत्कालिक पहचान दे सकने के कारण—अस्पर्श। उसे छेड़ सकने का अधिकार लेखक का कहाँ रहता है !
यह संस्करण....
अपनी-पुस्तकों के नए संस्करण खुशी देते हैं पर कुछ नई तरह की चुनौतियाँ भी पैदा करते हैं। अपना लिखा हुआ चूँकि दूर जा चुका होता है इसलिए अपने को एक पाठकीय बाहरीपन में पढ़ना भी सम्भव लगने लगता है। कथा की निहित सम्भावनाओं को दूसरी तरह से देखने का यह अवसर सदा प्रीतिकर ही लगे—ऐसा निश्चय से नहीं कहा जा सकता। यह स्थिति एक तरह की कातरता भी पैदा करती है क्योंकि तब तक तो हम दूसरे समय में दाखिल हो चुकते हैं। वहाँ पाठक तो रचना के उपलब्ध रूप को पढ़ता है पर रचनाकार उतनी दूरी के बावजूद मूल अनुभव और रचना के स्मृत अवलोकन को भी साथ-साथ पढ़ता है। इस पुनर्पाठ के समय कितने ही नए परिप्रेक्ष्य उस संरचना में जगह पा जाने की पेशकश कर रहे हैं, जो उपद्रवी ज्यादा लगते हैं। अपने समय और स्थिति से अनुभव का रिश्ता चाहे कितना भी ईमानदार और प्रामाणिक रहा हो पर इस प्रक्रिया में अपने ही मन्तव्यों के बीच फाँक दिखाई देने लगती है, जिसे रचनाकार की विकास-यात्रा के खाते में डाला जरूर जा सकता है पर इस बारे में कोई मानक टिप्पणी नहीं की जा सकती ; क्योंकि अधिकारपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि इसे विकासशीलता ही कहेंगे या गतिशीलता के नियम की अपनी अनिवार्यता। तिस पर तुर्रा यह कि फैसला तो समय और पाठक के हाथ में ही रहने को है इसलिए अपना देखना अपने छोर का यथाशक्ति अन्वेषण करना भर ही है, वह भी रचना में छेड़छाड़ के अधिकार से रहित।
किसी रोपी हुई रचना को नई जमीन पर रोपना समय और जीवन-प्रवाह के अनगिनत अदृश्य आयामों की सत्ता और रूपान्तरण के सच को भूल जाने के दुस्साहस जैसा है। इस अहसास के चलते ऐसा कुछ न करने की चेतनागत मजबूरी लगातार मेरे साथ रही। वैसी स्वीकृति मुझे अपने भीतर से नहीं मिल पाती रही अतः जो कुछ है यथातथ्य है। इतना ज़रूर है कि पुस्तक के नए संस्करण के समय अन्य पाठकों के साथ लेखक नाम का एक और पाठक भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाता है।
एक पाठक की तरह इन कहानियों के पुनर्पाठ ने कुछ आत्ममुग्धता दी होती तो शायद ज्यादा अच्छा लगता, फिलहाल तो यह मेरे लिए पाठकीय आस्वाद और नए संस्करण की ज़रूरत से उपजे सुखद अवसर को छू लेने की घड़ी है।
किसी रोपी हुई रचना को नई जमीन पर रोपना समय और जीवन-प्रवाह के अनगिनत अदृश्य आयामों की सत्ता और रूपान्तरण के सच को भूल जाने के दुस्साहस जैसा है। इस अहसास के चलते ऐसा कुछ न करने की चेतनागत मजबूरी लगातार मेरे साथ रही। वैसी स्वीकृति मुझे अपने भीतर से नहीं मिल पाती रही अतः जो कुछ है यथातथ्य है। इतना ज़रूर है कि पुस्तक के नए संस्करण के समय अन्य पाठकों के साथ लेखक नाम का एक और पाठक भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाता है।
एक पाठक की तरह इन कहानियों के पुनर्पाठ ने कुछ आत्ममुग्धता दी होती तो शायद ज्यादा अच्छा लगता, फिलहाल तो यह मेरे लिए पाठकीय आस्वाद और नए संस्करण की ज़रूरत से उपजे सुखद अवसर को छू लेने की घड़ी है।
समान्तर चलते हुए
दरवाजे के नीचे की दरार से न जाने कितनी तेजी़ से डाकिए ने सरकाया था पत्र कि ज़रा-सी गोंद के सहारे चिपका लिफा़फा़ अपने-आप खुल गया और उसमें कैद काग़ज की तहें बाहर झाँकने लगीं। उठाते-उठाते उसमें से कुछ खिसककर नीचे गिर गया। देखा—पान के पत्तों के आकार के मोटे काग़ज पर काटे गए दो पत्ते, परन्तु आपस में जुड़े हुए। स्पष्ट था, ये पत्ते ह्रदय का आकार इंगित कर रहे हैं। एक पर लिखा था ‘यू’ और दूसरे पर ‘आई’। लिफा़फा़ पलटकर देखा, नाम मिलिन्द का ही था।
एक हल्का सा आमोद-भाव, जो पत्तों के आकार को देखकर भीतर से उठा था, एकाएक ठहर गया। पत्र हाथ में लिये मैं आया और अपनी मेज़ पर बैठ गया। कुछ क्षण तक उसे उलट-पलटकर देखता रहा। स्वाभाविक था कि लिफा़फा़ खुल गया है तो उस पत्र को पढ़ने लगूँ, परन्तु अपने भीतर एक अनचीन्हा भय पहचान पा रहा था। किस चीज़ से डर रहा था मैं ? ...किसी बात के स्थापित हो जाने से.. पर क्यों ?
साधारणतया इस घर में कोई किसी के पत्र नहीं पढ़ता। अचानक हाथ पड़ जाएँ तो भी नहीं। निजता के प्रति सम्मान इस घर में एक तरह से शुरू से ही चलता आ रहा है। एक सीमा तक तो व्यक्ति सबका होता है, परन्तु एक सीमा के बाद किसी का नहीं। अपने-आपके साथ हो पाना हर किसी की उत्कट आवश्यकता है, जिसका अतिक्रमण किसी हालत में नहीं किया जाना चाहिए ; ऐसा मैं हमेशा से समझता और समझाता आया हूँ।
मज़मून हाथों में लेकर मैं इसे उलटता-पलटता हूँ। मैंने इसे नहीं खोला, यह खुल गया है। मेरी इसे पढ़ने में कोई गहरी रुचि नहीं है—परन्तु उत्सुकता अवश्य है। इसमें क्या लिखा हो सकता है, इसका मुझे कुछ-कुछ अनुमान भी है—कुछ ऐसी बातें जो हर कोई अपने जीवन में कभी-न-कभी किसी रूप में दोहराता है, पर सोचता है कि वही इसे पहली बार सोच या महसूस कर रहा है।
पत्र का सम्बोधन था, ‘माई लव !’ विनोद का एक भाव उभरते-उभरते कहीं भीतर ही दब जाता है। मैं अकारण अपने को गम्भीर होते पाता हूँ।
पत्र में वह सब था, जो किसी को अपनत्व और निकटता का एहसास दे सके। चाह, व्यग्रता, पिघलन, आत्मीयता, कुछ चुने हुए समर्पित वाक्यांश। मधुरता का उफान उठाते हुए। मैं उसे एक ही साँस में पढ़ गया और फिर एक स्थल पर अनायास टिक गया।
‘तुम्हारे होने से मैं अत्यन्त सुरक्षित महसूस करती हूँ।’’
‘तुम्हारे होने से मैं अत्यन्त सुरक्षित महसूस करती हूँ,’ ये शब्द सारे मज़मून से छिटककर अलग जा पड़े और मुझे घेरने से लगे।
ये शब्द क्या मिलिन्द के हैं ? मेरे बच्चे के लिए ? जिसे अभी तक, कुछ समय पहले तक, मैं अबोध समझता था ? जिसको पालने-पोसने, खिलाने-पिलाने और पढ़ाने-लिखाने के उत्तरदायित्व से अपने को अब तक मुक्त नहीं समझता था ? वही मिलिन्द ? वह अबोध शिशु ?
अभी कल ही की तो बातें हैं, सपनों की तरह द्वारों की चौखटों पर अटकी हुईं। अनीता से विवाह..गहन उन्माद और मादकता में डुबो देनेवाले सुख—देह पिघलाती गरमाइयाँ और मन को सराबोर करती गहराइयाँ—तन, मन की पूर्णता में हिलोर लेते तीन वर्ष...फिर दो के स्वप्नों को नया अर्थ देनेवाले एक तीसरे के आने की सम्भावना। उससे संलग्न स्वप्न और जीवन के चम्बे-चौड़े नक्शों की आयोजना...नियति की कुटिलता से अनजान जाने कितनी अपेक्षाएँ, जिसमें न केवल भविष्य, बल्कि जन्म-जन्मान्तर के साथ ही प्रतिबद्धताएँ भी उजागर थीं।
और फिर सुमधुर अपेक्षाओं को क्रूरता से रौंदता एक दिन—एम्बुलेंस, अस्पताल, डॉक्टरों के चिन्ता से गहराते चेहरे। इमरजेंसी में उभरे आई नर्सों की सतर्क तत्परता। साँस में दारुण कष्ट...एक न टूटनेवाली बेहोशी...अन्ततः विषैले हो गए अनीता के रक्त से केवल मिलिन्द की ही रक्षा की जा सकी।
मेरी अप्रस्तुत क्षमता पर उत्तदायित्व का एक पहाड़ रखकर वह चली गई।...भयाकुलता और घटनाओं की वेगमयता के कारण मैं खुलकर रो भी न सका था। अनिश्चित भविष्य और बोझिल दायित्व के समक्ष भौंचक्का खड़ा रह गया था।
दूसरी शादी की बात भी उसी समय उठाई गई थी। मैं उदासीन ही रहा। मामी और दीदी कुछ-कुछ समय रहकर वापस चली गई थीं। दीदी ने औपचारिक, परन्तु प्रच्छन्न सतर्कता से तरल होते हुए कहा था, ‘‘बेबी को मैं ले जाती हूँ, कुछ सँभल जाने पर तू ले आना।’’ केनवास की लम्बी कुर्सी पर शिथिल पड़ा मैं थोड़ी देर उनको जाँचता रहा था। फिर स्वयं ही कह दिया था, ‘‘अभी रहने दो, दीदी !’’
दीदी वह दृष्टि सहन न कर सकी थीं। दीदी को दोष नहीं देता। उनकी अपनी परिस्थितियों में ऐसा कर पाना असम्भव था। विरोधी भावों की धूप-छाँह में वह न केवल अपना कर्तव्य स्थिर कर रही थी, मैं भी उसी क्षण जीवन का अर्थघटन कर रहा था—कर्तव्य-के-नाम होम होते रहना। उस समय मेरे मन में उस मांस के लोथड़े के लिए—जो अपनी जीवित तथता में मेरे हाथ थमा दिया गया था—कितना वात्सल्य था, इसे मैं तटस्थ बैठा बराबर तौलता रहा था। अपने को मैंने उस समय एक कसैली दयनीयता के आधीन पाया था। मैं शायद जीवन की चारुता निभाने के पक्ष में था।
सब धीरे-धीरे चले गए। एक-एक करके। केवल मैं रह गया, एक खुरदरे यथार्थ के सामने। हर किसी का एक ही सुझाव कि मैं गृहस्थी बसा डालूँ, विवाह कर डालूँ—परन्तु मैं अपने अतल में पिघलती दुविधाओं का कभी समाधान न कर सका।
समझ ही नहीं पाया कि नए सपनों की अपेक्षाओं में जीती कुँआरी संवेदना के प्रत्युत्तर ढूँढ़ती किसी नवोढ़ा को मैं कैसे एक पराए वात्सल्य से लाद दूँ ! क्या यह एक भावनात्मक बलात्कार न होगा ?
और यह भी कि अतीत की मुट्ठी में भिंची अनीता के साथ बिताए अभिन्न अन्तरंग क्षणों के स्मरण की कोर भी मुझसे झटकी न गई। एक नैतिक किस्म का ममत्व उस स्मरण के प्रति मन में बना रहा।
यों तो जीवन में मैं कभी तथाकथित नैतिक दबावों से संचालित नहीं रहा—बल्कि जीवन के बाहरी कलेवर से जुड़ी नैतिक वर्जनाओं के प्रति एक उपेक्षा ही मेरे मन में रही है—फिर भी अपनी तह से, किन्हीं नैतिक मान्यताओं का उपासक जरूर रहा हूँ। मैंने जीवन को व्यक्तित्व और परिवेश के बीच समायोजन की कोशिश की तरह देखना चाहा है। जिसमें सहज मानसिक ईमानदारी एक जरूरी शर्त लगती रही है। इसीलिए मैं आन्तरिक शर्तों को नकार नहीं सका, आवश्यकता के दबाव में भी नहीं। ‘कठिनाई हुई तो सोचूँगा,’ यही सोचता रहा। ‘मिलिन्द के लिए अत्यावश्यक हो गया तो विचार करूँगा,‘ पर बात टलती गई। अधिक वेतन पर जुटाए नौकरों की तत्परता और अपने सजग ममत्व के बीच मिलिन्द एक अच्छे सिंचे हुए पौधे की तरह पनपता गया और घर भी बँधी स्थिर चाल से चलता रहा।
एक मैं ही था (मुझे अचानक बोध हुआ) जो किनारों से दूर बहता अपनी पहचान के घेरे से बाहर चला आया था। लगने लगा था, ऐसे स्थल पर खड़ा हूँ, जहाँ बीहड़ विस्तृत रेगिस्तान है, अकेलापन है, अकुलाहट है, रीते दरीचों से गुजरने वाली हवा का शोर है, और कुछ नहीं। बहुत ध्यान से देखने पर लगता, दूर-बहुत दूर-एक मन्द-सी लौ-सा प्रतीत है, एक निर्वैक्तिक वर्तमान और एक अनिश्चित भविष्य...मिलिन्द बड़ा हो चला है। सिर पर ओढ़ा हु्आ मिंशन जैसे पूरा हो चला है। अब ? जीवन चुपचाप खिसक चला है, कुछ बटोरने जैसा अभी बचा है क्या ? रीते हाथ...खाली हाथ ?....
धक्का-सा लगा था उस दिन। ‘‘आपको पता है डैडी ! इस महीने की इक्कीस तारीख को मैं एडल्ट हो जाऊँगा,’’ मिलिन्द ने खाना खाते समय हँसकर कहा था।
मैं चौंक गया था। क्यों चौंका ? किसी दूसरे आसमान से उठकर तो नहीं आई थी यह बात। मेरे देखते-देखते मेरे ठीक सामने घटती रही थी अठारह साल-एक-दर-एक अठारह साल।
‘‘बहुत अच्छे,’’मैंने उत्साह दिखाया था पर ठहाके की उस हँसी के साथ पहली बार उस पर अपने अधिकार के ढीलेपन का एक प्रच्छन्न सा भाव भी कौंधा था। मिलिन्द...एडल्ट ?
‘‘यह दिन हम खूब धूमधाम से मनाएँगे,’’ कहकर दोशाला समेटता हुआ मैं अपनी स्टडी में चला आया था। रीतेपन की जो किरच इधर कई सालों से अस्तित्व में सरकती आ रही है, अधिक चुभने लगी थी।
पता नहीं कितनी रात तक तिपाई पर पैर फैलाए मैं निश्चल बैठा रहा था। वह कब का सो चुका था, मैं कब से जाग रहा था। एक छोटी सी स्थिति हम दोनों पर अलग-अलग ढंग से घट रही थी। उसकी ओर मेरी जरूरतों में इधर कोई संगति नहीं रह गई थी।
शाम को घर लौटते वक्त एक अनिच्छा अपनी उग्रता में मन में धरना देकर बैठ जाती थी। मालूम होता—वह घर पर नहीं होगा। टेनिस खेलने गया होगा। वहाँ से लाइब्रेरी। वहाँ से अनिल के घर। घर में होता भी तो जिसकी दिनचर्या और अपनी –जरूरत में तालमेल बिठाना मुश्किल होता है। वह जितना ही स्वतन्त्र, सन्तुष्ट और आत्मविश्वासी हो रहा था, उस पर अपने मानसिक अवलम्बन के कारण मैं उतना ही टूटता जा रहा था। एक ही स्थिति उसकी उपलब्धि थी, मेरी नियति।
न जाने कैसे इतना ठहराव और सूनापन जीवन में सरक आया। रीतेपन की विभीषिका हर एकान्त में प्रतिध्वनित होने लगी।
अब सोचता हूँ तो लगता है कि इसी, अवश्य इसी मनः स्थिति ने ही जीवन के वर्तमान अध्याय को जन्म दिया होगा। आज इस समय मिलिन्द के नाम का पत्र हाथ में पकड़े-पकड़े मुझे अनायास मंजुला के शब्द याद आ रहे हैं, ‘तुम्हारे होने से मैं अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ।’
अपने अधपके बालों में उँगलियाँ फिराते शरारत-भरी दुष्टता के साथ मैं उससे कहता हूँ, ‘‘मेरे साथ ? कब्र में पैर लटकाकर बैठे इस बूढ़े के साथ ? तुम्हारी पसन्द की दाद नहीं दे सकता।’’ वह हँसती है और कहती है कि मैं उसकी दृष्टि से देखने की क्षमता नहीं रखता।
मैं बार-बार सोचा करता हूँ, क्या मंजुला मेरे एकान्त की ऊब से उपजी अस्त-व्यस्त मनःस्थिति की तलाश है ? या अनायास रास्ते में मिल गई कोई मणि ? परन्तु उत्तर नहीं पाता। उत्तर आवश्यक भी नहीं लगता।
उसके साथ रहते प्रश्नों का हजूम टल जाता है अपने-आप। अपने ‘कुछ’ होने का, अपने को स्थापित करने का, उसकी अस्मिता के प्रति सजग होने का भाव अधिक उभरता है। उसके साथ रहकर लगता है, मैं जीवन के प्रवाह में तैर रहा हूँ, अकेला तट पर खड़ा लहरें नहीं गिन रहा। उसके साथ हर आवाज़ सार्थक लगती है, खोखला शोर नहीं।
इस सबके बावजूद हमने कोई भविष्य निश्चित नहीं किया। एक-दूसरे पर अपने अधिकार को हड़पकर जेब में रख लेने की आतुरता हमारे मन में नहीं उग पाई। मुझे तो खैर आदत-सी पड़ गई है, अप्राप्ति के अन्तहीन फैलाव में अपनी नन्ही सी प्राप्ति को कृपण की तरह पकड़े रहने की। परन्तु वह भी कुछ नहीं कहती। मेरे और अपने संयुक्त भविष्य का कोई प्रश्न भूलकर भी मेरे सामने नहीं रखती। ऐसा कोई आग्रह उसकी ओर से नहीं आता।
वह समझती है, यह बहुत सम्भव नहीं है उसकी परिस्थितियों में। ऐसे विपन्न समय में वह अपने को अपने परिवार से विलगाकर नहीं आ सकती। पक्षाघात से पीड़ित और वर्षों से घरवालों की सेवा-सुश्रूषा पर आश्रित पिता, युद्ध की भेंट गया बड़ा भाई, दो छोटी बहनें ; जिनका लिखना-पढ़ना जारी था।
जीविकोपार्जन की मशीन बनकर, घर की सिरमौर होकर वह एक ऊँचाई पर स्थिर बैठी है। उसे उपलब्धियाँ वर्जित नहीं, दिशा और मंजि़ल वर्जित है। अपनी धुरी पर कायम रहकर पैसे कमाती हुई वह कुछ भी करे, जीवन को किसी भी दृष्टिकोण से देखे-इससे किसी को कुछ लेना-देना न था। वह घर की एक अविच्छिन्न आर्थिक नियति थी, जिसे अलगाना एक आर्थिक प्रश्न अधिक था।
इसीलिए उसने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने भी उससे कभी कुछ नहीं पूछा। अत्यन्त भीतर से जन्में आवेगों के आलोक में हम हर बार एक-दूसरे को पहले से अधिक पहचानते रहे हैं और निशब्द निकटता को समर्पित होते रहे हैं।
वह अपने को आलोड़ित नदी के वक्ष पर एक डगमगाती किश्ती-सा महसूस करती है, जिसे किनारे की आशा नहीं, अतः तलाश नहीं। पर उसे पतवार सँभालनेवाले केवट का सहारा तो चाहिए ही कि प्रवंचनाओं के तटों से टकराए नहीं, टूट न जाए। हम दोनों के बीच की स्थिति बहाव की एक स्थिति है-तरल, अबाध, पर दिशाहीन। तिस पर भी वह बार-बार कहती है कि मेरे होने से वह अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करती है।
मेरे ? मैं ? मैं जो उसका भविष्य नहीं रच सकता, उसे उसकी मारक नियति से निजात नहीं दिला सकता, उसे उसके परिवेश से तोड़कर नए भविष्य की परिकल्पना नहीं भेंट कर सकता, उसकी लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकता। एक ऐसा मैं ! उसके साथ-वह कहती है-वह सुरक्षित महसूस करती है ! कैसे कह पाती है वह !
आज...आज कोई और भी, किसी और से कुछ ऐसा ही कह रहा है, ‘वह सुरक्षित महसूस करती है उसके साथ’ किसके साथ ? मिलिन्द के साथ ? मेरे बच्चे के साथ ? जिसके दूध की कच्ची गन्ध और पेशाब का गर्म गीलापन मैं अभी तक अपने कपड़ों में महसूस कर सकता हूँ। जिसकी खिलखिलाती हँसी की आहट वर्षों की सलवटों में से झाँकती आज भी मेरे एकान्त से खेल उठती है। वही मिलिन्द ! मेरा बच्चा ! सुरक्षा के कन्धे बढ़ाता हुआ किसी का अवलम्ब बन रहा है ! क्या सचमुच ?
मैंने उठकर पत्र बन्द करके चुपके से मिलिन्द की मेज पर रख दिया। उदास हूँ या थक गया हूँ, मुझे नहीं मालूम। आज शायद पहली बार मैं अपने को इतना बड़ा महसूस कर रहा हूँ।
मुझे ध्यान आता है कि एक पीढ़ी के संघर्षों का अभी समाधान नहीं हुआ, दूसरी उसमें कदम रख चुकी है।
तुम्हारे होने से...मिलिन्द...अपनी नियति को शायद वह हमसे अच्छा झेल सके...शायद।
एक हल्का सा आमोद-भाव, जो पत्तों के आकार को देखकर भीतर से उठा था, एकाएक ठहर गया। पत्र हाथ में लिये मैं आया और अपनी मेज़ पर बैठ गया। कुछ क्षण तक उसे उलट-पलटकर देखता रहा। स्वाभाविक था कि लिफा़फा़ खुल गया है तो उस पत्र को पढ़ने लगूँ, परन्तु अपने भीतर एक अनचीन्हा भय पहचान पा रहा था। किस चीज़ से डर रहा था मैं ? ...किसी बात के स्थापित हो जाने से.. पर क्यों ?
साधारणतया इस घर में कोई किसी के पत्र नहीं पढ़ता। अचानक हाथ पड़ जाएँ तो भी नहीं। निजता के प्रति सम्मान इस घर में एक तरह से शुरू से ही चलता आ रहा है। एक सीमा तक तो व्यक्ति सबका होता है, परन्तु एक सीमा के बाद किसी का नहीं। अपने-आपके साथ हो पाना हर किसी की उत्कट आवश्यकता है, जिसका अतिक्रमण किसी हालत में नहीं किया जाना चाहिए ; ऐसा मैं हमेशा से समझता और समझाता आया हूँ।
मज़मून हाथों में लेकर मैं इसे उलटता-पलटता हूँ। मैंने इसे नहीं खोला, यह खुल गया है। मेरी इसे पढ़ने में कोई गहरी रुचि नहीं है—परन्तु उत्सुकता अवश्य है। इसमें क्या लिखा हो सकता है, इसका मुझे कुछ-कुछ अनुमान भी है—कुछ ऐसी बातें जो हर कोई अपने जीवन में कभी-न-कभी किसी रूप में दोहराता है, पर सोचता है कि वही इसे पहली बार सोच या महसूस कर रहा है।
पत्र का सम्बोधन था, ‘माई लव !’ विनोद का एक भाव उभरते-उभरते कहीं भीतर ही दब जाता है। मैं अकारण अपने को गम्भीर होते पाता हूँ।
पत्र में वह सब था, जो किसी को अपनत्व और निकटता का एहसास दे सके। चाह, व्यग्रता, पिघलन, आत्मीयता, कुछ चुने हुए समर्पित वाक्यांश। मधुरता का उफान उठाते हुए। मैं उसे एक ही साँस में पढ़ गया और फिर एक स्थल पर अनायास टिक गया।
‘तुम्हारे होने से मैं अत्यन्त सुरक्षित महसूस करती हूँ।’’
‘तुम्हारे होने से मैं अत्यन्त सुरक्षित महसूस करती हूँ,’ ये शब्द सारे मज़मून से छिटककर अलग जा पड़े और मुझे घेरने से लगे।
ये शब्द क्या मिलिन्द के हैं ? मेरे बच्चे के लिए ? जिसे अभी तक, कुछ समय पहले तक, मैं अबोध समझता था ? जिसको पालने-पोसने, खिलाने-पिलाने और पढ़ाने-लिखाने के उत्तरदायित्व से अपने को अब तक मुक्त नहीं समझता था ? वही मिलिन्द ? वह अबोध शिशु ?
अभी कल ही की तो बातें हैं, सपनों की तरह द्वारों की चौखटों पर अटकी हुईं। अनीता से विवाह..गहन उन्माद और मादकता में डुबो देनेवाले सुख—देह पिघलाती गरमाइयाँ और मन को सराबोर करती गहराइयाँ—तन, मन की पूर्णता में हिलोर लेते तीन वर्ष...फिर दो के स्वप्नों को नया अर्थ देनेवाले एक तीसरे के आने की सम्भावना। उससे संलग्न स्वप्न और जीवन के चम्बे-चौड़े नक्शों की आयोजना...नियति की कुटिलता से अनजान जाने कितनी अपेक्षाएँ, जिसमें न केवल भविष्य, बल्कि जन्म-जन्मान्तर के साथ ही प्रतिबद्धताएँ भी उजागर थीं।
और फिर सुमधुर अपेक्षाओं को क्रूरता से रौंदता एक दिन—एम्बुलेंस, अस्पताल, डॉक्टरों के चिन्ता से गहराते चेहरे। इमरजेंसी में उभरे आई नर्सों की सतर्क तत्परता। साँस में दारुण कष्ट...एक न टूटनेवाली बेहोशी...अन्ततः विषैले हो गए अनीता के रक्त से केवल मिलिन्द की ही रक्षा की जा सकी।
मेरी अप्रस्तुत क्षमता पर उत्तदायित्व का एक पहाड़ रखकर वह चली गई।...भयाकुलता और घटनाओं की वेगमयता के कारण मैं खुलकर रो भी न सका था। अनिश्चित भविष्य और बोझिल दायित्व के समक्ष भौंचक्का खड़ा रह गया था।
दूसरी शादी की बात भी उसी समय उठाई गई थी। मैं उदासीन ही रहा। मामी और दीदी कुछ-कुछ समय रहकर वापस चली गई थीं। दीदी ने औपचारिक, परन्तु प्रच्छन्न सतर्कता से तरल होते हुए कहा था, ‘‘बेबी को मैं ले जाती हूँ, कुछ सँभल जाने पर तू ले आना।’’ केनवास की लम्बी कुर्सी पर शिथिल पड़ा मैं थोड़ी देर उनको जाँचता रहा था। फिर स्वयं ही कह दिया था, ‘‘अभी रहने दो, दीदी !’’
दीदी वह दृष्टि सहन न कर सकी थीं। दीदी को दोष नहीं देता। उनकी अपनी परिस्थितियों में ऐसा कर पाना असम्भव था। विरोधी भावों की धूप-छाँह में वह न केवल अपना कर्तव्य स्थिर कर रही थी, मैं भी उसी क्षण जीवन का अर्थघटन कर रहा था—कर्तव्य-के-नाम होम होते रहना। उस समय मेरे मन में उस मांस के लोथड़े के लिए—जो अपनी जीवित तथता में मेरे हाथ थमा दिया गया था—कितना वात्सल्य था, इसे मैं तटस्थ बैठा बराबर तौलता रहा था। अपने को मैंने उस समय एक कसैली दयनीयता के आधीन पाया था। मैं शायद जीवन की चारुता निभाने के पक्ष में था।
सब धीरे-धीरे चले गए। एक-एक करके। केवल मैं रह गया, एक खुरदरे यथार्थ के सामने। हर किसी का एक ही सुझाव कि मैं गृहस्थी बसा डालूँ, विवाह कर डालूँ—परन्तु मैं अपने अतल में पिघलती दुविधाओं का कभी समाधान न कर सका।
समझ ही नहीं पाया कि नए सपनों की अपेक्षाओं में जीती कुँआरी संवेदना के प्रत्युत्तर ढूँढ़ती किसी नवोढ़ा को मैं कैसे एक पराए वात्सल्य से लाद दूँ ! क्या यह एक भावनात्मक बलात्कार न होगा ?
और यह भी कि अतीत की मुट्ठी में भिंची अनीता के साथ बिताए अभिन्न अन्तरंग क्षणों के स्मरण की कोर भी मुझसे झटकी न गई। एक नैतिक किस्म का ममत्व उस स्मरण के प्रति मन में बना रहा।
यों तो जीवन में मैं कभी तथाकथित नैतिक दबावों से संचालित नहीं रहा—बल्कि जीवन के बाहरी कलेवर से जुड़ी नैतिक वर्जनाओं के प्रति एक उपेक्षा ही मेरे मन में रही है—फिर भी अपनी तह से, किन्हीं नैतिक मान्यताओं का उपासक जरूर रहा हूँ। मैंने जीवन को व्यक्तित्व और परिवेश के बीच समायोजन की कोशिश की तरह देखना चाहा है। जिसमें सहज मानसिक ईमानदारी एक जरूरी शर्त लगती रही है। इसीलिए मैं आन्तरिक शर्तों को नकार नहीं सका, आवश्यकता के दबाव में भी नहीं। ‘कठिनाई हुई तो सोचूँगा,’ यही सोचता रहा। ‘मिलिन्द के लिए अत्यावश्यक हो गया तो विचार करूँगा,‘ पर बात टलती गई। अधिक वेतन पर जुटाए नौकरों की तत्परता और अपने सजग ममत्व के बीच मिलिन्द एक अच्छे सिंचे हुए पौधे की तरह पनपता गया और घर भी बँधी स्थिर चाल से चलता रहा।
एक मैं ही था (मुझे अचानक बोध हुआ) जो किनारों से दूर बहता अपनी पहचान के घेरे से बाहर चला आया था। लगने लगा था, ऐसे स्थल पर खड़ा हूँ, जहाँ बीहड़ विस्तृत रेगिस्तान है, अकेलापन है, अकुलाहट है, रीते दरीचों से गुजरने वाली हवा का शोर है, और कुछ नहीं। बहुत ध्यान से देखने पर लगता, दूर-बहुत दूर-एक मन्द-सी लौ-सा प्रतीत है, एक निर्वैक्तिक वर्तमान और एक अनिश्चित भविष्य...मिलिन्द बड़ा हो चला है। सिर पर ओढ़ा हु्आ मिंशन जैसे पूरा हो चला है। अब ? जीवन चुपचाप खिसक चला है, कुछ बटोरने जैसा अभी बचा है क्या ? रीते हाथ...खाली हाथ ?....
धक्का-सा लगा था उस दिन। ‘‘आपको पता है डैडी ! इस महीने की इक्कीस तारीख को मैं एडल्ट हो जाऊँगा,’’ मिलिन्द ने खाना खाते समय हँसकर कहा था।
मैं चौंक गया था। क्यों चौंका ? किसी दूसरे आसमान से उठकर तो नहीं आई थी यह बात। मेरे देखते-देखते मेरे ठीक सामने घटती रही थी अठारह साल-एक-दर-एक अठारह साल।
‘‘बहुत अच्छे,’’मैंने उत्साह दिखाया था पर ठहाके की उस हँसी के साथ पहली बार उस पर अपने अधिकार के ढीलेपन का एक प्रच्छन्न सा भाव भी कौंधा था। मिलिन्द...एडल्ट ?
‘‘यह दिन हम खूब धूमधाम से मनाएँगे,’’ कहकर दोशाला समेटता हुआ मैं अपनी स्टडी में चला आया था। रीतेपन की जो किरच इधर कई सालों से अस्तित्व में सरकती आ रही है, अधिक चुभने लगी थी।
पता नहीं कितनी रात तक तिपाई पर पैर फैलाए मैं निश्चल बैठा रहा था। वह कब का सो चुका था, मैं कब से जाग रहा था। एक छोटी सी स्थिति हम दोनों पर अलग-अलग ढंग से घट रही थी। उसकी ओर मेरी जरूरतों में इधर कोई संगति नहीं रह गई थी।
शाम को घर लौटते वक्त एक अनिच्छा अपनी उग्रता में मन में धरना देकर बैठ जाती थी। मालूम होता—वह घर पर नहीं होगा। टेनिस खेलने गया होगा। वहाँ से लाइब्रेरी। वहाँ से अनिल के घर। घर में होता भी तो जिसकी दिनचर्या और अपनी –जरूरत में तालमेल बिठाना मुश्किल होता है। वह जितना ही स्वतन्त्र, सन्तुष्ट और आत्मविश्वासी हो रहा था, उस पर अपने मानसिक अवलम्बन के कारण मैं उतना ही टूटता जा रहा था। एक ही स्थिति उसकी उपलब्धि थी, मेरी नियति।
न जाने कैसे इतना ठहराव और सूनापन जीवन में सरक आया। रीतेपन की विभीषिका हर एकान्त में प्रतिध्वनित होने लगी।
अब सोचता हूँ तो लगता है कि इसी, अवश्य इसी मनः स्थिति ने ही जीवन के वर्तमान अध्याय को जन्म दिया होगा। आज इस समय मिलिन्द के नाम का पत्र हाथ में पकड़े-पकड़े मुझे अनायास मंजुला के शब्द याद आ रहे हैं, ‘तुम्हारे होने से मैं अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ।’
अपने अधपके बालों में उँगलियाँ फिराते शरारत-भरी दुष्टता के साथ मैं उससे कहता हूँ, ‘‘मेरे साथ ? कब्र में पैर लटकाकर बैठे इस बूढ़े के साथ ? तुम्हारी पसन्द की दाद नहीं दे सकता।’’ वह हँसती है और कहती है कि मैं उसकी दृष्टि से देखने की क्षमता नहीं रखता।
मैं बार-बार सोचा करता हूँ, क्या मंजुला मेरे एकान्त की ऊब से उपजी अस्त-व्यस्त मनःस्थिति की तलाश है ? या अनायास रास्ते में मिल गई कोई मणि ? परन्तु उत्तर नहीं पाता। उत्तर आवश्यक भी नहीं लगता।
उसके साथ रहते प्रश्नों का हजूम टल जाता है अपने-आप। अपने ‘कुछ’ होने का, अपने को स्थापित करने का, उसकी अस्मिता के प्रति सजग होने का भाव अधिक उभरता है। उसके साथ रहकर लगता है, मैं जीवन के प्रवाह में तैर रहा हूँ, अकेला तट पर खड़ा लहरें नहीं गिन रहा। उसके साथ हर आवाज़ सार्थक लगती है, खोखला शोर नहीं।
इस सबके बावजूद हमने कोई भविष्य निश्चित नहीं किया। एक-दूसरे पर अपने अधिकार को हड़पकर जेब में रख लेने की आतुरता हमारे मन में नहीं उग पाई। मुझे तो खैर आदत-सी पड़ गई है, अप्राप्ति के अन्तहीन फैलाव में अपनी नन्ही सी प्राप्ति को कृपण की तरह पकड़े रहने की। परन्तु वह भी कुछ नहीं कहती। मेरे और अपने संयुक्त भविष्य का कोई प्रश्न भूलकर भी मेरे सामने नहीं रखती। ऐसा कोई आग्रह उसकी ओर से नहीं आता।
वह समझती है, यह बहुत सम्भव नहीं है उसकी परिस्थितियों में। ऐसे विपन्न समय में वह अपने को अपने परिवार से विलगाकर नहीं आ सकती। पक्षाघात से पीड़ित और वर्षों से घरवालों की सेवा-सुश्रूषा पर आश्रित पिता, युद्ध की भेंट गया बड़ा भाई, दो छोटी बहनें ; जिनका लिखना-पढ़ना जारी था।
जीविकोपार्जन की मशीन बनकर, घर की सिरमौर होकर वह एक ऊँचाई पर स्थिर बैठी है। उसे उपलब्धियाँ वर्जित नहीं, दिशा और मंजि़ल वर्जित है। अपनी धुरी पर कायम रहकर पैसे कमाती हुई वह कुछ भी करे, जीवन को किसी भी दृष्टिकोण से देखे-इससे किसी को कुछ लेना-देना न था। वह घर की एक अविच्छिन्न आर्थिक नियति थी, जिसे अलगाना एक आर्थिक प्रश्न अधिक था।
इसीलिए उसने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने भी उससे कभी कुछ नहीं पूछा। अत्यन्त भीतर से जन्में आवेगों के आलोक में हम हर बार एक-दूसरे को पहले से अधिक पहचानते रहे हैं और निशब्द निकटता को समर्पित होते रहे हैं।
वह अपने को आलोड़ित नदी के वक्ष पर एक डगमगाती किश्ती-सा महसूस करती है, जिसे किनारे की आशा नहीं, अतः तलाश नहीं। पर उसे पतवार सँभालनेवाले केवट का सहारा तो चाहिए ही कि प्रवंचनाओं के तटों से टकराए नहीं, टूट न जाए। हम दोनों के बीच की स्थिति बहाव की एक स्थिति है-तरल, अबाध, पर दिशाहीन। तिस पर भी वह बार-बार कहती है कि मेरे होने से वह अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करती है।
मेरे ? मैं ? मैं जो उसका भविष्य नहीं रच सकता, उसे उसकी मारक नियति से निजात नहीं दिला सकता, उसे उसके परिवेश से तोड़कर नए भविष्य की परिकल्पना नहीं भेंट कर सकता, उसकी लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकता। एक ऐसा मैं ! उसके साथ-वह कहती है-वह सुरक्षित महसूस करती है ! कैसे कह पाती है वह !
आज...आज कोई और भी, किसी और से कुछ ऐसा ही कह रहा है, ‘वह सुरक्षित महसूस करती है उसके साथ’ किसके साथ ? मिलिन्द के साथ ? मेरे बच्चे के साथ ? जिसके दूध की कच्ची गन्ध और पेशाब का गर्म गीलापन मैं अभी तक अपने कपड़ों में महसूस कर सकता हूँ। जिसकी खिलखिलाती हँसी की आहट वर्षों की सलवटों में से झाँकती आज भी मेरे एकान्त से खेल उठती है। वही मिलिन्द ! मेरा बच्चा ! सुरक्षा के कन्धे बढ़ाता हुआ किसी का अवलम्ब बन रहा है ! क्या सचमुच ?
मैंने उठकर पत्र बन्द करके चुपके से मिलिन्द की मेज पर रख दिया। उदास हूँ या थक गया हूँ, मुझे नहीं मालूम। आज शायद पहली बार मैं अपने को इतना बड़ा महसूस कर रहा हूँ।
मुझे ध्यान आता है कि एक पीढ़ी के संघर्षों का अभी समाधान नहीं हुआ, दूसरी उसमें कदम रख चुकी है।
तुम्हारे होने से...मिलिन्द...अपनी नियति को शायद वह हमसे अच्छा झेल सके...शायद।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i