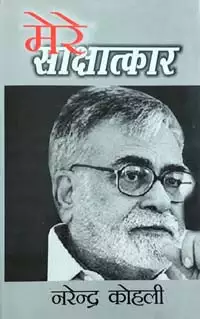|
बहुभागीय पुस्तकें >> महासमर - बंधन महासमर - बंधननरेन्द्र कोहली
|
142 पाठक हैं |
|||||||
नरेन्द्र कोहली का उपन्यास -‘महासमर’ घटनाएँ तथा पात्र महाभारत से संबद्ध हैं, किन्तु यह कृति एक उपन्यास है-आज के एक लेखक का मौलिक सृजन!
इस पुस्तक का सेट खरीदें।
Bandhan - a hindi book by Narendra Kohli - बंधन - नरेन्द्र कोहली
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रख्यात कथाओं का पुनर्सृजन उन कथाओं का संशोधन अथवा पुनर्लेखन नहीं होता वह उनका युग सापेक्ष अनुकूलन मात्र भी नहीं होता। पीपल के बीज से उत्पन्न प्रत्येक वृक्ष पीपल होते हुए भी, स्वयं में एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह न किसी का अनुसरण है, न किसी का नया संस्करण ! मौलिक उपन्यास का भी यही सत्य है।
मानवता के शाश्वत प्रश्नों का साक्षात्कार लेखक अपने गली मुहल्ले, नगर देश, समाचार-पत्रों तथा समकालीन इतिहास में आबद्ध होकर भी करता है, और मानव सभ्यता तथा संस्कृति की सम्पूर्ण जातीय स्मृति के सम्मुख बैठकर भी। पौराणिक उपन्यासकार के ‘प्राचीन’ में घिरकर प्रगति के प्रति अंधे हो जाने की संभावना उतनी ही घातक है, जितनी समकालीन लेखक की समसामयिक पत्रकारिता में बंदी हो एक खण्ड सत्य को पूर्ण सत्य मानने की मूढ़ता। सृजक साहित्यकार का सत्य अपने काल-खण्ड का अंग होते हुए भी, खंडों के अतिक्रमण का लक्ष्य लेकर चलता है।
नरेन्द्र कोहली का नया उपन्यास है ‘महासमर’ घटनाएँ तथा पात्र महाभारत से संबद्ध हैं, किन्तु यह कृति का एक उपन्यास है-आज के एक लेखक का मौलिक सृजन !
मानवता के शाश्वत प्रश्नों का साक्षात्कार लेखक अपने गली मुहल्ले, नगर देश, समाचार-पत्रों तथा समकालीन इतिहास में आबद्ध होकर भी करता है, और मानव सभ्यता तथा संस्कृति की सम्पूर्ण जातीय स्मृति के सम्मुख बैठकर भी। पौराणिक उपन्यासकार के ‘प्राचीन’ में घिरकर प्रगति के प्रति अंधे हो जाने की संभावना उतनी ही घातक है, जितनी समकालीन लेखक की समसामयिक पत्रकारिता में बंदी हो एक खण्ड सत्य को पूर्ण सत्य मानने की मूढ़ता। सृजक साहित्यकार का सत्य अपने काल-खण्ड का अंग होते हुए भी, खंडों के अतिक्रमण का लक्ष्य लेकर चलता है।
नरेन्द्र कोहली का नया उपन्यास है ‘महासमर’ घटनाएँ तथा पात्र महाभारत से संबद्ध हैं, किन्तु यह कृति का एक उपन्यास है-आज के एक लेखक का मौलिक सृजन !
बन्धन
यह असम्भव था।
घटना से पूर्व तो इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी; घटित हो जाने के बाद भी देवव्रत को इसका विश्वास ही नहीं था। ऐसा सम्भव कैसे था ?....
‘असम्भव ! असम्भव !’ मन-ही-मन देवव्रत ने अनेक बार दुहराया। पर राजा शान्तनु का रथ जा चुका था- सत्य यही था।
हस्तिनापुर का नगर-द्वार ‘वर्द्धमान’ नव-वधू के समान सजाया गया था। राज्य के उच्च अधिकारी और असंख्य सामान्य जन, राजा की अगवानी के लिए नगर-द्वार पर उपस्थित थे। और उस सारे समुदाय के शीर्ष पर थे-देवव्रत ! देवव्रत अधिकारी नहीं, प्रजा नहीं-पुत्र थे ! शान्तनु के एकमात्र पुत्र ! और रुकना तो दूर, राजा का रथ तनिक धीमा भी नहीं हुआ। राजा ने चलते हुए रथ में से भी खड़े होकर अधिकारियों और प्रजा का अभिवादन स्वीकार करने का कष्ट नहीं किया। किसी ने राजा की एक झलक भी नहीं देखी। रथ का कोई गवाक्ष नहीं खुला, कोई यवनिका नहीं हिली।
अहंकार !
प्रजा की इतनी उपेक्षा। यही अहंकार राजवंशों को खा जाता है।.... प्रजा और अधिकारियों को भूल भी जाये तो देवव्रत तो पुत्र हैं...राजा शान्तनु उनके पिता हैं। कैसे पिता हैं शान्तनु ?.....
देवव्रत की आँखों के सामने अपना शैशव घूम गया। पिता को छोड़कर माता अलग हो गयी थीं। इस विलगाव के कारण उन दोनों में से किसको कितनी पीड़ा हुई, यह देवव्रत नहीं जानते- पर स्वयं अपनी पीड़ा को वे कभी नहीं भूल पाये। प्रत्येक बालक के माता-पिता दोनों हैं- उनके माता-पिता, होकर भी नहीं थे। देवव्रत ने सदा यही पाया था कि न माँ सहज थीं, न पिता। माँ चाहती थीं कि देवव्रत पिता के पास रहें, ताकि पुरुकुल के योग्य उनका लालन-पालन हो और पिता कुछ इतने उद्भ्रान्त थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं था कि उनका एक पुत्र भी है। पत्नी से वंचित होने की पीड़ा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि अपने पुत्र को वे कितना वंचित कर रहे हैं। ...देवव्रत का शैशव, बालावस्था, किशोरावस्था, तरुणाई-वय के ये सारे खण्ड विभिन्न ऋषियों के साथ उनके आश्रमों के कठोर अनुशासन में कट गये। तपस्वी गुरुओं कठोर अनुशासन के निबद्ध कर्तव्यमिश्रित स्नेह उन्हें बहुत मिला, किन्तु माता-पिता का सर्वक्षमाशील वात्सल्य...
और तभी से देवव्रत के मन में परिवार, समाज और संसार को लेकर अनेक प्रश्न उठते रहे हैं।....परिवार क्या है ? पति-पत्नी का परस्पर आकर्षण एक-दूसरे को सम्मान और स्वतन्त्रता देने में है या अपने सुख के लिए अन्य प्राणी को अपनी इच्छाओं का दास बना लेने में ? यदि दूसरे पक्ष के सुख के लिए स्वयं को खपा देना परिवार का आधार है तो दूसरे पक्ष की कामना ही क्यों होती है ? स्त्री-पुरुष विवाह क्यों करते हैं- अपनी रिक्ति को भरने के लिए या दूसरे पक्ष के अभावों को दूर करने के लिए, या परस्पर एक-दूसरे का सहारा बन, अपनी-अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए ?....वात्सल्य क्या है ? व्यक्ति, सन्तान अपने सुख के लिए माँगता है ? बालक को खिलौना का सुख कभी अभीष्ट नहीं। माता-पिता सन्तान के लिए स्वयं को नहीं तपाते-वे तपते हैं तो अपने अभावों से तपते हैं। खिलौना टूट जाये तो बच्चा इसलिए नहीं रोता कि खिलौने को टूटकर कष्ट हुआ होगा, वह इसलिए रोता है कि उसकी सम्पत्ति नष्ट हो गयी है जिसे खेलकर उसे सुख मिलता था, वह आधार नष्ट हो गया है।...
देवव्रत के मन में प्रश्नों के हथौड़े चलते ही रहते हैं-सन्तान-सुख,..वात्सल्य सुख..सुख है क्या ? अपनी सुविधा को सुख मानते हैं या अपने अहंकार की पुष्टि को या मन की अनुकूलता को ? देवव्रत अपने मन की प्रतिकूलता को बहुत जल्दी अनुकूलता में बदल लेते हैं। किन्तु बात देवव्रत की नहीं है बात तो राजा शान्तनु की है ....
....माता के द्वारा पिता को सौंप दिए जाने के पश्चात से राजा शान्तनु उनकी ओर कुछ उन्मुख हुए थे। देवव्रत को लगने लगा था कि वात्सल्य के कुछ छींटे उन पर भी पड़े थे। गृहस्थी के सुख की कुछ कल्पना उनके मन में भी जागने लगी थी। परिजनों के सम्बन्धों को सामाजिक आवश्यकता और कर्तव्य से हटकर भावात्मक स्तर पर वे भी देखने लगे थे- पर ऐसे ही समय में पिता की ओर से यह उपेक्षा....देवव्रत के हाथ, पिता के चरण-स्पर्श के लिए उठे ही रह गये। पिता का रथ रुका ही नहीं...
देवव्रत का मन क्षुब्ध होकर जैसे उन पर धिक्कार बरसाने लगा था। वे किसी से कोई अपेक्षा करते ही क्यों हैं ? वे अपने भीतर ही सम्पूर्णता क्यों नहीं खोज लेते ? क्या आवश्यकता है उन्हें, किसी के प्यार की ? पिता ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा तो क्या और नहीं फेरा तो क्या ? ये अपेक्षाएँ ही तो अन्ततः निराशा को जन्म देती हैं और निराशा दुख का कारण बनती है। दुख से बचना है तो अपेक्षाओं से बचना होगा...उनका मन एक बार सदा के लिए क्यों नहीं मान लेता कि जीवन, मात्र एक कठोर कर्तव्य है- जिसका निर्वाह करना ही पड़ता है। यह स्नेह, प्यार, वात्सल्य...ये सब तो समयानुसार ओढ़े गये छल-छद्म मात्र हैं, जो दूसरों को भी धोखा देते हैं और स्वयं अपने लिए भी छलों का प्रसाद खड़ा कर लेते हैं। पिता को
अपनी पत्नी प्रिय थी, इसलिए उसके मोह में अपने होंठों को सिए बैठे रहे। माँ ने एक पश्चात एक कर, सात पुत्रों को गंगा में बहा दिया। पिता के मन में वात्सल्य होता, तो माँ का हाथ न पकड़ लेते ?.. हाँ ! देवव्रत की बारी आयी तो उन्होंने माँ का हाथ पकड़ा भी था ? पर पत्नी से दूर होने का इतना शोक हुआ उन्हें कि उनका एक पुत्र अभी जीवित भी था..जिस पुत्र की रक्षा के लिए पत्नी की इच्छा के प्रतिकूल चले थे....उसी पुत्र को भूल गये। उन्हें कभी ध्यान भी आया कि देवव्रत कहाँ हैं ?.... जीवित भी है या पत्नी के वियोग में पगला कर...
देवव्रत का प्रवाह अटका....आज उनका भी तो व्यवहार उन्मत्त का-सा ही था,.....कहीं पिता अस्वस्थ तो नहीं हैं ?... स्थितियाँ बदलते ही सारे निष्कर्ष बदल जाते हैं। यदि राजा सचमुच अस्वस्थ हैं, तो प्रजा द्वारा अपना स्वागत देखने के लिए वे कैसे रुकते। रोगी के लिए या प्रजा का अभिनन्दन व्यवहार आवश्यक नहीं होता। शिष्टाचार के नियम उसके लिए नहीं होतेः औपचारिकता की अपेक्षा नहीं की जाती।....यदि ऐसा न होता, तो देवव्रत को खड़े देखकर भी सारथि वल्गा न खींचता और रथ हाँककर ले जाता ? .....असम्भव !
आत्मलीन देवव्रत अपने रथ तक आये।
‘‘चलो।’’ उन्होंने सारथि को आदेश दिया, ‘‘पिताजी के पास।’’
एक क्षण के लिए उनके मन में आया भी कि अधिकारियों और प्रजा से भी कह दें कि राजा अस्वस्थ हैं।....पर बिना किसी प्रमाण के ऐसी बात कैसे कही जा सकती है। यह तो उनका अनुमान मात्र था। पहले उनको पिता का आचरण दम्भपूर्ण लग रहा था, अब एक उन्मत्त या रोगी का-सा। .....जाने सच्चाई क्या है।..पिता अस्वस्थ हों, उन्मत्त हों, क्षुब्ध हों... वे सारे सम्बन्धों से उदासीन हो उठते हैं.... पता नहीं पिता का मन-तुरंग एक दिशा में ही क्यों सरपट भागता है। उसके सुम के नीचे एक हल्की-सी कंकड़ी भी आ जाये तो उसका सारा सन्तुलन बिगड़ जाता है। फिर वह न तो अपनी दिशा में ही अग्रसर हो सकता है और न किसी और दिशा का ध्यान उसे रहता है। पीठ के बल, भूमि पर पड़ा हुआ चारों टाँगें आकाश की ओर उठाये, झटके खाता और देता रहता है, उसके मुख से यातना के सीत्कार ही फूटते हैं....
जब पिता, माँ के मोह में पड़े थे...पता नहीं, वह प्रेम था या मोह ! क्या
अन्तर है प्रेम और मोह में ?....कभी-कभी देवव्रत को मोह, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति...सब अलग-अलग मूर्तिमान होते दिखाई देते हैं और कभी सब गड्डमड्ड हो जाते हैं..... इस समय तो वे यह भी स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि यह पिता का प्रासाद था या उन्माद...ऐसी अस्पष्ट-सी स्थिति में देवव्रत राज्य के अधिकारियों को क्या कह सकते हैं। वे लोग अपने राजा की अगवानी के लिए आये थे। राजा आ चुके हैं। नगर में प्रवेश कर चुके हैं। सम्भवतः इस समय अपने महल में होंगे। यदि थोड़ी देर रुककर उन्होंने प्रजा का अभिवादन स्वीकार कर लिया होता तो प्रजा उनका जय-जयरकार कर, उनपर पुष्प-वर्षा कर अपने-अपने घर लौट जाती।.....राजा रुके नहीं हैं, तो प्रजा लौट तो जायेगी ही।
देवव्रत को लगा, वे स्वयं भी सहज नहीं हो पा रहे हैं। उनके भीतर के द्वन्द्व और असमंजस, उन्हें कुछ स्पष्ट निर्णय नहीं करने देते और वे निष्क्रियता के भी अनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं। सम्भव है कि इस समय उनके इस प्रकार चुपचाप चले जाने के विषय में भी पीछे टीका-टिप्पणी हो रही हो। लोग राजा शान्तनु के आचरण के स्थान पर उन्हीं के आचरण की समीक्षा कर रहे हों।
पर अब देवव्रत लौट नहीं सकते थे उनका रथ काफी आगे बढ़ आया था।
घटना से पूर्व तो इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी; घटित हो जाने के बाद भी देवव्रत को इसका विश्वास ही नहीं था। ऐसा सम्भव कैसे था ?....
‘असम्भव ! असम्भव !’ मन-ही-मन देवव्रत ने अनेक बार दुहराया। पर राजा शान्तनु का रथ जा चुका था- सत्य यही था।
हस्तिनापुर का नगर-द्वार ‘वर्द्धमान’ नव-वधू के समान सजाया गया था। राज्य के उच्च अधिकारी और असंख्य सामान्य जन, राजा की अगवानी के लिए नगर-द्वार पर उपस्थित थे। और उस सारे समुदाय के शीर्ष पर थे-देवव्रत ! देवव्रत अधिकारी नहीं, प्रजा नहीं-पुत्र थे ! शान्तनु के एकमात्र पुत्र ! और रुकना तो दूर, राजा का रथ तनिक धीमा भी नहीं हुआ। राजा ने चलते हुए रथ में से भी खड़े होकर अधिकारियों और प्रजा का अभिवादन स्वीकार करने का कष्ट नहीं किया। किसी ने राजा की एक झलक भी नहीं देखी। रथ का कोई गवाक्ष नहीं खुला, कोई यवनिका नहीं हिली।
अहंकार !
प्रजा की इतनी उपेक्षा। यही अहंकार राजवंशों को खा जाता है।.... प्रजा और अधिकारियों को भूल भी जाये तो देवव्रत तो पुत्र हैं...राजा शान्तनु उनके पिता हैं। कैसे पिता हैं शान्तनु ?.....
देवव्रत की आँखों के सामने अपना शैशव घूम गया। पिता को छोड़कर माता अलग हो गयी थीं। इस विलगाव के कारण उन दोनों में से किसको कितनी पीड़ा हुई, यह देवव्रत नहीं जानते- पर स्वयं अपनी पीड़ा को वे कभी नहीं भूल पाये। प्रत्येक बालक के माता-पिता दोनों हैं- उनके माता-पिता, होकर भी नहीं थे। देवव्रत ने सदा यही पाया था कि न माँ सहज थीं, न पिता। माँ चाहती थीं कि देवव्रत पिता के पास रहें, ताकि पुरुकुल के योग्य उनका लालन-पालन हो और पिता कुछ इतने उद्भ्रान्त थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं था कि उनका एक पुत्र भी है। पत्नी से वंचित होने की पीड़ा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि अपने पुत्र को वे कितना वंचित कर रहे हैं। ...देवव्रत का शैशव, बालावस्था, किशोरावस्था, तरुणाई-वय के ये सारे खण्ड विभिन्न ऋषियों के साथ उनके आश्रमों के कठोर अनुशासन में कट गये। तपस्वी गुरुओं कठोर अनुशासन के निबद्ध कर्तव्यमिश्रित स्नेह उन्हें बहुत मिला, किन्तु माता-पिता का सर्वक्षमाशील वात्सल्य...
और तभी से देवव्रत के मन में परिवार, समाज और संसार को लेकर अनेक प्रश्न उठते रहे हैं।....परिवार क्या है ? पति-पत्नी का परस्पर आकर्षण एक-दूसरे को सम्मान और स्वतन्त्रता देने में है या अपने सुख के लिए अन्य प्राणी को अपनी इच्छाओं का दास बना लेने में ? यदि दूसरे पक्ष के सुख के लिए स्वयं को खपा देना परिवार का आधार है तो दूसरे पक्ष की कामना ही क्यों होती है ? स्त्री-पुरुष विवाह क्यों करते हैं- अपनी रिक्ति को भरने के लिए या दूसरे पक्ष के अभावों को दूर करने के लिए, या परस्पर एक-दूसरे का सहारा बन, अपनी-अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए ?....वात्सल्य क्या है ? व्यक्ति, सन्तान अपने सुख के लिए माँगता है ? बालक को खिलौना का सुख कभी अभीष्ट नहीं। माता-पिता सन्तान के लिए स्वयं को नहीं तपाते-वे तपते हैं तो अपने अभावों से तपते हैं। खिलौना टूट जाये तो बच्चा इसलिए नहीं रोता कि खिलौने को टूटकर कष्ट हुआ होगा, वह इसलिए रोता है कि उसकी सम्पत्ति नष्ट हो गयी है जिसे खेलकर उसे सुख मिलता था, वह आधार नष्ट हो गया है।...
देवव्रत के मन में प्रश्नों के हथौड़े चलते ही रहते हैं-सन्तान-सुख,..वात्सल्य सुख..सुख है क्या ? अपनी सुविधा को सुख मानते हैं या अपने अहंकार की पुष्टि को या मन की अनुकूलता को ? देवव्रत अपने मन की प्रतिकूलता को बहुत जल्दी अनुकूलता में बदल लेते हैं। किन्तु बात देवव्रत की नहीं है बात तो राजा शान्तनु की है ....
....माता के द्वारा पिता को सौंप दिए जाने के पश्चात से राजा शान्तनु उनकी ओर कुछ उन्मुख हुए थे। देवव्रत को लगने लगा था कि वात्सल्य के कुछ छींटे उन पर भी पड़े थे। गृहस्थी के सुख की कुछ कल्पना उनके मन में भी जागने लगी थी। परिजनों के सम्बन्धों को सामाजिक आवश्यकता और कर्तव्य से हटकर भावात्मक स्तर पर वे भी देखने लगे थे- पर ऐसे ही समय में पिता की ओर से यह उपेक्षा....देवव्रत के हाथ, पिता के चरण-स्पर्श के लिए उठे ही रह गये। पिता का रथ रुका ही नहीं...
देवव्रत का मन क्षुब्ध होकर जैसे उन पर धिक्कार बरसाने लगा था। वे किसी से कोई अपेक्षा करते ही क्यों हैं ? वे अपने भीतर ही सम्पूर्णता क्यों नहीं खोज लेते ? क्या आवश्यकता है उन्हें, किसी के प्यार की ? पिता ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा तो क्या और नहीं फेरा तो क्या ? ये अपेक्षाएँ ही तो अन्ततः निराशा को जन्म देती हैं और निराशा दुख का कारण बनती है। दुख से बचना है तो अपेक्षाओं से बचना होगा...उनका मन एक बार सदा के लिए क्यों नहीं मान लेता कि जीवन, मात्र एक कठोर कर्तव्य है- जिसका निर्वाह करना ही पड़ता है। यह स्नेह, प्यार, वात्सल्य...ये सब तो समयानुसार ओढ़े गये छल-छद्म मात्र हैं, जो दूसरों को भी धोखा देते हैं और स्वयं अपने लिए भी छलों का प्रसाद खड़ा कर लेते हैं। पिता को
अपनी पत्नी प्रिय थी, इसलिए उसके मोह में अपने होंठों को सिए बैठे रहे। माँ ने एक पश्चात एक कर, सात पुत्रों को गंगा में बहा दिया। पिता के मन में वात्सल्य होता, तो माँ का हाथ न पकड़ लेते ?.. हाँ ! देवव्रत की बारी आयी तो उन्होंने माँ का हाथ पकड़ा भी था ? पर पत्नी से दूर होने का इतना शोक हुआ उन्हें कि उनका एक पुत्र अभी जीवित भी था..जिस पुत्र की रक्षा के लिए पत्नी की इच्छा के प्रतिकूल चले थे....उसी पुत्र को भूल गये। उन्हें कभी ध्यान भी आया कि देवव्रत कहाँ हैं ?.... जीवित भी है या पत्नी के वियोग में पगला कर...
देवव्रत का प्रवाह अटका....आज उनका भी तो व्यवहार उन्मत्त का-सा ही था,.....कहीं पिता अस्वस्थ तो नहीं हैं ?... स्थितियाँ बदलते ही सारे निष्कर्ष बदल जाते हैं। यदि राजा सचमुच अस्वस्थ हैं, तो प्रजा द्वारा अपना स्वागत देखने के लिए वे कैसे रुकते। रोगी के लिए या प्रजा का अभिनन्दन व्यवहार आवश्यक नहीं होता। शिष्टाचार के नियम उसके लिए नहीं होतेः औपचारिकता की अपेक्षा नहीं की जाती।....यदि ऐसा न होता, तो देवव्रत को खड़े देखकर भी सारथि वल्गा न खींचता और रथ हाँककर ले जाता ? .....असम्भव !
आत्मलीन देवव्रत अपने रथ तक आये।
‘‘चलो।’’ उन्होंने सारथि को आदेश दिया, ‘‘पिताजी के पास।’’
एक क्षण के लिए उनके मन में आया भी कि अधिकारियों और प्रजा से भी कह दें कि राजा अस्वस्थ हैं।....पर बिना किसी प्रमाण के ऐसी बात कैसे कही जा सकती है। यह तो उनका अनुमान मात्र था। पहले उनको पिता का आचरण दम्भपूर्ण लग रहा था, अब एक उन्मत्त या रोगी का-सा। .....जाने सच्चाई क्या है।..पिता अस्वस्थ हों, उन्मत्त हों, क्षुब्ध हों... वे सारे सम्बन्धों से उदासीन हो उठते हैं.... पता नहीं पिता का मन-तुरंग एक दिशा में ही क्यों सरपट भागता है। उसके सुम के नीचे एक हल्की-सी कंकड़ी भी आ जाये तो उसका सारा सन्तुलन बिगड़ जाता है। फिर वह न तो अपनी दिशा में ही अग्रसर हो सकता है और न किसी और दिशा का ध्यान उसे रहता है। पीठ के बल, भूमि पर पड़ा हुआ चारों टाँगें आकाश की ओर उठाये, झटके खाता और देता रहता है, उसके मुख से यातना के सीत्कार ही फूटते हैं....
जब पिता, माँ के मोह में पड़े थे...पता नहीं, वह प्रेम था या मोह ! क्या
अन्तर है प्रेम और मोह में ?....कभी-कभी देवव्रत को मोह, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति...सब अलग-अलग मूर्तिमान होते दिखाई देते हैं और कभी सब गड्डमड्ड हो जाते हैं..... इस समय तो वे यह भी स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि यह पिता का प्रासाद था या उन्माद...ऐसी अस्पष्ट-सी स्थिति में देवव्रत राज्य के अधिकारियों को क्या कह सकते हैं। वे लोग अपने राजा की अगवानी के लिए आये थे। राजा आ चुके हैं। नगर में प्रवेश कर चुके हैं। सम्भवतः इस समय अपने महल में होंगे। यदि थोड़ी देर रुककर उन्होंने प्रजा का अभिवादन स्वीकार कर लिया होता तो प्रजा उनका जय-जयरकार कर, उनपर पुष्प-वर्षा कर अपने-अपने घर लौट जाती।.....राजा रुके नहीं हैं, तो प्रजा लौट तो जायेगी ही।
देवव्रत को लगा, वे स्वयं भी सहज नहीं हो पा रहे हैं। उनके भीतर के द्वन्द्व और असमंजस, उन्हें कुछ स्पष्ट निर्णय नहीं करने देते और वे निष्क्रियता के भी अनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं। सम्भव है कि इस समय उनके इस प्रकार चुपचाप चले जाने के विषय में भी पीछे टीका-टिप्पणी हो रही हो। लोग राजा शान्तनु के आचरण के स्थान पर उन्हीं के आचरण की समीक्षा कर रहे हों।
पर अब देवव्रत लौट नहीं सकते थे उनका रथ काफी आगे बढ़ आया था।
2
पिता के महल का वातावरण प्रवास से लौटे राजा के घर-जैसा नहीं था। उनसे मिलने आये मन्त्रियों, सेनापतियों, कुटुम्बियों और सेवकों की भीड़ वहाँ नहीं थी। उल्लास का खुला वातावरण भी नहीं था। मौन का तनाव कुछ अधिक कठोरता से व्याप्त था।
देवव्रत तेज डगों से चलते हुए द्वारपाल तक आये, ‘‘पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करो।’’
चाहकर भी उनके मुख से ‘चक्रवर्ती’, सम्राट’ या ‘राजा’ जैसा शब्द नहीं निकला था। उनके ममत्व अपने पिता के लिए आन्दोलित था, चक्रवर्ती की चिन्ता उन्हें नहीं थी।
‘‘युवराज !’’ द्वारपाल का स्वर अनुशासनबद्ध न होकर आत्मीय था, ‘‘चक्रवर्ती स्वस्थ नहीं हैं।’’
देवव्रत का अनुमान ठीक ही था। वस्तुतः पिता स्वस्थ नहीं थे। द्वारपाल उनका प्रणाम निवेदित करने के लिए भीतर नहीं जा रहा था। सम्भवतः उसे ऐसा ही आदेश दिया गया था। किन्तु, वह उन्हें भीतर जाने से रोक भी नहीं रहा था।
यदि पिता ने किसी के भी प्रवेश का निषेध किया है तो द्वारपाल का कर्तव्य है कि उन्हें भीतर जाने से रोके; और यदि पिता ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है तो उसे चाहिए कि भीतर जाकर उनका प्रणाम निवेदित करे....पर देवव्रत की तर्क-श्रृंखला यहीं रुक गयी। उन्हें लगा कि द्वारपाल के मन में भी कुछ स्पष्ट नहीं है। यहाँ सब कुछ अस्पष्ट है। ऐसी अस्पष्टता और द्वन्द्व की स्थिति में बेचारा द्वारपाल भी क्या करेगा-यही न कि न स्वयं भीतर जाने का साहस कर पायेगा और न उन्हें रोकने की धृष्टता....
‘‘राजवैध को सूचना दी गयी क्या ?’’
‘‘नहीं!’’
‘‘क्यों ?’’
सम्भवतः चक्रवर्ती का यही आदेश है।’’
देवव्रत कुछ सोचते हुए से खड़े रहे।
‘‘अमात्य कहाँ हैं ?’’ सहसा उन्होंने पूछा।
‘‘वे चक्रवर्ती के साथ यहाँ नहीं आये थे।’’
देवव्रत का माथा ठनकाः अमात्य क्यों नहीं आये ? वे पिता के साथ गये थे। वे अवश्य जानते होंगे कि पिता अस्वस्थ हैं। वे क्यों नहीं आये ? और राजवैद्य क्यों नहीं बुलाये गये ?....
अनुमान से ये सब कुछ नहीं जाना जा सकता । पिता से साक्षात्कार करना ही होगा।
देवव्रत ने कक्ष में प्रवेश किया।
पिता थके हुए-से, या असहाय रोगी के समान नहीं लौटे थे। वे अपने पलंग पर औधें मुँह पड़े थे। पहली दृष्टि में तो देवव्रत को लगा कि शायद पिता रो रहे हैं और स्वयं को सँभालने के प्रयत्न में ही बिस्तर पर औंधे हो गये हैं...देवव्रत के पग पृथ्वी पर चिपक गये। कितने कष्ट में हैं पिता। हस्तिनापुर के चक्रवर्ती, पुरुराज, वीरवर शान्तनु अपने कक्ष में अकेले पड़े
असहाय-से रो रहे हैं....मनुष्य कोई भी क्यों न हो-बलवान, ज्ञानी, चक्रवर्ती...आखिर मनुष्य है। शरीर और मन ने नियमों का दास। संसार के सुख-दुख से मुक्ति नहीं है उसकी। ...तो फिर जीवन में वह सुख-दुख मानता ही क्यों है ? वह जीवन को कार्य-कारण के नियमों के अधीन क्यों नहीं समझता ? जब यह सब अवश्यंभावी है तो इतने हाथ-पैर पटकने से क्या लाभ ? क्यों लपकता है मनुष्य लोभ और लाभ की ओर ? क्या पा जायेगा वह उसमें ? चक्रवर्ती शान्तनु स्वयं अपनी इच्छा से सुख पाने के लिए मृगया के लिए गये थे। क्या सुख मिला ? पड़े हुए आहत मृग के समान हाथ-पैर पटक रहे हैं कैसी पीड़ा है पिता को ? कहीं आखेट में कोई गहरा घाव तो नहीं खा गये ? पर नहीं। पिता शारीरिक घाव खाकर उसकी पीड़ा से रोनेवालों में से नहीं हैं। और यदि वैसा होता तो अमात्य साथ आये होते और इस समय यहाँ वैद्यों और शल्य चिकित्सकों का जमघट लगा होता.....
सहसा शान्तनु ने करवट बदली और जैसे अपनी किसी भीतरी पीड़ा से विविश होकर, उन्होंने अपने वक्ष पर दो-तीन घूँसे लगाये, मानो किसी उठते हुए आवेग को दबा रहे हों। उनका गहरा निःश्वास उनकी पीड़ा का भी प्रतीत था और उत्तेजना का भी। उन्होंने अपने समूचे शरीर को अकड़या और सारे संयम और नियन्त्रण के बावजूद अपनी दोनों टाँगें उठाकर पलंग पर पटक दीं। लगा वे अभी नियमित रूप से छटपटाते हुए हाथ-पैर पटकने लगेंगे।
तो पिता शीरीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं थे- देवव्रत ने सोचा-उनका मन उद्विग्न था। पर है तो उद्विग्नता भी रोग ही.....
‘‘पिताजी !’’ देवव्रत ने आगे बढ़, पिता के चरण छुए।
शान्तनु ने न उठकर पुत्र को गले से लगाया, न कोई आशीष दी। लोकाचार के अभ्यास की बाध्याता थी जैसे, अपनी हथेली देवव्रत के सिर पर रख दी।
देवव्रत ने देखा, पिता के चेहरे पर पीड़ा के तनाव की स्पष्ट रेखाएँ थीं। एक लम्बे प्रवास के बाद पुत्र को देखकर भी उनकी आँखों में वात्सल्य तो क्या एक हल्का-सा औपचारिक हास भी नहीं उतरा था। विचित्र भाव थे पिता की आकृति परः कभी ताप से दग्ध होते हुए निरीह जीव की पराजय कभी उग्र मानसिकता की दिग्दाह करने की व्यग्र हिंसा। दोनों में से एक भी भाव कुछ अधिक क्षणों तक टिक नहीं पाता था।....
देवव्रत को लगा, वे पिता से अपनी अवहेलना की शिकायत नहीं कर पायेंगे। इस प्रकार पीड़ा में तड़पना, मनुष्य दूसरों की भावना का क्या सम्मान कर पायेगा।..., फिर देवव्रत ने तो बहुत पहले ही स्वयं को समझा लिया था कि वे अपने पिता से .....पिता से क्या, किसी से भी कोमलता और स्नेह की कोई अपेक्षा नहीं करेंगे।
‘‘आप अस्वस्थ हैं पिताजी ?’’
शान्तनु ने एक क्षण के लिए स्थिर दृष्टि से पुत्र की ओर देखा और फिर जैसे सायास, अस्त-व्यस्त-से उठे खड़े हुए। अपने उत्तरीय को ठीक करने की व्यस्तता में इधर-उधर टलहते हुए, वे उत्तर को टालते रहे। देवव्रत के मन में जिज्ञासा जागीः थोड़ी-थोड़ी देर के लिए उभरनेवाला अपने प्रति उपालम्भ का वह हल्का-सा आभास....पर उपालम्भ का कारण ?
‘‘अस्वस्थ नहीं हूँ पुत्र !’’ शान्तनु अपना मन कुछ स्थिर करके बोले, ‘‘चिन्तित हूँ...चिन्ता से पीड़ित हूँ। चिन्ता की चिता का दाह सह रहा हूँ।’’ देवव्रत के मन में आया, कहें, ‘‘पिताजी ! आप उदभ्रान्त लगते हैं। आपका आचरण....।’’ पर देवव्रत ने कुछ कहा नहीं।
‘‘राजवैद्य को सूचना क्यों नहीं दी गयी पिताजी ?’’
‘‘कोई लाभ नहीं।’’
‘‘कारण जान सकता हूँ ?’’ देवव्रत का स्वर अत्यन्त विनीत था।
‘‘मुझे रोग नहीं, क्षोभ है। मेरी चिन्ता का समाधान वैद्य के पास नहीं है।’’
‘‘चक्रवर्ती सम्राटों को भी चिन्ताएँ होती हैं क्या?’’ देवव्रत को लगा, अपने मन से पूछा गया यह प्रश्न असावधानीवश उनके मुख से सशब्द निकल गया था। पर प्रश्न का दूसरा भाग उन्होंने अपने मन में ही रोक लिया था, ‘चिन्ताओं को दूर नहीं कर सकते तो ये सम्राज्य फिर किस काम के हैं ?’
शान्तनु ने पुत्र को नये सिरे से देखाः यह देवव्रत अनेक बार क्षत्रिय राजपुत्रों के समान नहीं, वनवासी वैरागियों के समान बातें करने लगता है। वनवासी ऋषियों के सान्निध्य में बिताया गया इसका आरम्भिक जीवन इसे राजपुत्रों की मानसिकता नहीं दे पाया है। शान्तनु को पहले इसका आभास हुआ तो वे पुत्र को आश्रमों में छोड़ने के स्थान पर, आचार्यों को ही राजमहल में बुला लेते।....न चाहते हुए भी वन वनवासियों के विरुद्ध उनका आक्रोश वाणी पा गया, ‘‘चक्रवर्ती सम्राटों को ही तो चिन्ताएँ होती हैं पुत्र ! कंगले वनवासियों के पास ऐसा होता ही क्या है, जिसकी वे चिन्ता करें।’’
‘‘अभाव की चिन्ता भी चिन्ता होती है पिताजी !’’ देवव्रत सहज भाव से बोले, ‘‘वरन् वह असुविधा भी होती है।’’
पर अधिकांश कथ्य, शब्दों के सहयोग के कारण उनके मन में ही रह गयाः यदि साम्राज्यों के साथ चिन्ताएँ ही जुड़ी हैं तो इतनी ललक से व्यक्ति साम्राज्य स्थापित करने के लिए लपकता ही क्यों है ? क्या मनुष्य इतनी-सी बात नहीं समझता कि उसका स्वार्थ किसमें है ? उसे किसका ग्रहण करना है, किसका त्याग ? यदि साम्राज्य चिन्ताओं का घर है तो मनुष्य को चाहिए कि उसे त्याज्य माने....
‘‘होगी ! ’’ शान्तनु ने उनकी बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वे अपनी चिन्ता में कहीं और गहरे उतर गये थे, ‘‘जाने क्यों गंगा ने मेरे सात पुत्रों को जीवन-मुक्त कर दिया....।
पिता जब भी इस घटना की ओर संकेत करते हैं, देवव्रत समझ नहीं पाते कि उनके मन में पत्नी की स्मृति जागी है या पुत्रों की। सात पुत्रों को जीवन-मुक्त करने वाले के लिए जो भाव पिता के मन में होना चाहिए था, उसका लेश मात्र भी शान्तनु के मन में नहीं था। कदाचित् उन सारी हृदय-विदारक घटनाओं के बाद भी आज तक उन्हें अपनी पत्नी के रूप की स्मृति मुग्ध करती थी। सन्तान को जीवन मुक्त करने वाली उस पत्नी से अब भी उन्हें वितृष्णा नहीं हुई थी। सन्तान भी उन्हें प्यारी रही होगी, तभी तो उन्होंने पत्नी को रुष्ट किया था; किन्तु सन्तान या पत्नी में से वे किसी एक को नहीं चाहते-दोनों को चाहते हैं। किन्तु यदि दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे वे ?....देवव्रत समझ नहीं पा रहे थे।
‘‘अब तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो।’’ शान्तनु पुनः बोले, ‘‘और मुझे बार-बार लगता है कि एक पुत्र का पिता, पुत्रहीन व्यक्ति से भी अधिक दुखी होता है।’’
‘‘क्यों पिताजी ?’’
‘‘पुत्र !’’ पहली बार शान्तनु का स्वर कुछ कोमल हुआ, ‘‘किसी मनुष्य के प्राण यदि एक निरीह और असहाय पक्षी में बन्द कर दिये जायें और पक्षी को स्वतन्त्र रूप से उड़ने के लिए मुक्त छोड़ दिया जाये तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी ?’’
देवव्रत ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पिता की बात पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
‘‘आकाश में गरुड़, श्येन तथा अन्य हिंस्र पक्षी हैं। धरती पर स्थान-स्थान पर बहेलिये के जाल बिछे हैं। किसी के लक्षित बाण या लक्ष्य-भ्रष्ट शस्त्र का वह निशाना हो सकता है।.... उस पक्षी की कोई हानि नहीं भी होती तो भी आशंकाओं के कारण उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, जिसके प्राण उसमें बन्द हैं; और यदि वह पक्षी मारा गया तो उस व्यक्ति का क्या होगा ?’’ शान्तनु ने जैसे उत्तर पाने के लिए देवव्रत की ओर देखा; और फिर स्वयं ही बोले, ‘‘तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो देवव्रत ! मेरे प्राण तुममें बसते हैं। तुम एक क्षण के लिए भी मुझसे विलग होते हो तो मेरी आत्मा व्याकुल हो उठती है....।
देवव्रत के मन में आया कि पिता का प्रतिवाद करें-यदि यह सच होता तो नगर-द्वार पर अगवानी के लिए आये खड़े पुत्र की अवहेलना कर पिता अपने महल में न आ गए होते। उसे स्वस्थ और प्रसन्न पाकर, उन्होंने उसे वहीं गले लगा लिया होता ...पुत्र इतना ही प्रिय था, तो उसे इस प्रकार नगर में अकेला छोड़कर नदियों के कछारों और बीहड़ वनों में मृगया का सुख पाने के लिए भटक न रहे होते।.... और अब, जब पुत्र सामने आया खड़ा है तो उसे उत्साहपूर्वक गले लगाकर सन्तोष प्रकट करने के स्थान पर, उद्विग्नता को गले लगाये न पड़े होते। पर देवव्रत ने यह सब कहा नहीं।
‘‘तुम शस्त्रधारी योद्धा हो पुत्र !’’ शान्तनु पहले की तुलना में कुछ आश्वस्त दिख रहे थे, ‘‘सदा युद्धों के लिए सन्नद्ध रहते हो। पर कुशल से कुशल योद्धा भी किसी-न-किसी दिन युद्ध में वीरगति पाता ही है। यदि किसी दिन तुम्हें वीरगति मिली तो मेरा क्या होगा पुत्र ? हस्तिनापुर के साम्राज्य का क्या होगा ? हमारे वंश का क्या होगा ? मेरी सद्गति कैसे होगी ?.....’’
देवव्रत के कान खड़े हो गये। क्या पिता विवाह का प्रस्ताव करनेवाले हैं ? क्या वंश-वृद्धि के नाम पर उनको घेरकर गृहस्थी की बेड़ियाँ पहनाना चाहते हैं। देवव्रत ने अपने शैशव में अपने माता-पिता के सम्बन्ध में, उनकी गृहस्थी के विषय में जो कुछ जाना और देखा-सुना है ...उसके बाद उनके मन में गृहस्थी के लिए कोई विशेष आकर्षण नहीं रह गया था।
अपनी माता और पिता की पीड़ा का लेशमात्र भी स्मरण होते ही, उनका मन इन सम्बन्धों से मुक्त होने के लिए पंख फड़फड़ाने लगता था। नारी का आकर्षण रूप भी देवव्रत के मन में कहीं वितृष्णा जगा जाता था...देवव्रत ने अपने भीतर कभी ऐसी रिक्ति का अनुभव नहीं किया, जिसे भरने के लिए उन्हें नारी के सान्निध्य की आवश्यकता हो। आज तक किसी नारी का रूप उसकी आँखों में नहीं उतरा, जो उसे रात भर जगाये रख सकता।...विवाह...अभी तो बार-बार उनका मन एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि व्यक्ति विवाह करता ही क्यों है ? शरीर सुख के लिए ? वंश-वृद्धि के लिए ? समाज और राष्ट्र के लिए ? किसके लिए है यह सारा हाहाकार ?......
‘‘गंगा के जाने के बाद मैंने दूसरा विवाह नहीं किया।’’ शान्तनु कह रहे थे, ‘‘आज भी नहीं करना चाहता। पर एक पुत्र....’’ उन्होंने रुककर देवव्रत को देखा, ‘‘जिसका पुत्र होता ही नहीं, उसे कुछ छिनने का भय नहीं होता, पर जिसका एक ही पुत्र हो, वह सदा उसके लिए...।
देवव्रत से पिता सहमत नहीं हो पा रहे थेः पिता को अपनी चिन्ता है या पुत्र की ? उनकी चिन्ता अपने लिए है या पुत्र के लिए ? उन्हें अपने पुत्र के लिए साम्राज्य चाहिए या अपने साम्राज्य के लिए पुत्र चाहिए ? अपना वंश वे क्यों चलाना चाहते हैं- अपनी सद्गति के लिए ?...पिता ने यह चिन्ता तो कभी नहीं की कि यदि उनका देहान्त हो गया तो उनके पुत्र का संरक्षक कौन होगा ? यदि राज्य नष्ट हो गया तो पुत्र के उपभोग के लिए सम्पत्ति कहाँ से आयेगी ?...
देवव्रत तेज डगों से चलते हुए द्वारपाल तक आये, ‘‘पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करो।’’
चाहकर भी उनके मुख से ‘चक्रवर्ती’, सम्राट’ या ‘राजा’ जैसा शब्द नहीं निकला था। उनके ममत्व अपने पिता के लिए आन्दोलित था, चक्रवर्ती की चिन्ता उन्हें नहीं थी।
‘‘युवराज !’’ द्वारपाल का स्वर अनुशासनबद्ध न होकर आत्मीय था, ‘‘चक्रवर्ती स्वस्थ नहीं हैं।’’
देवव्रत का अनुमान ठीक ही था। वस्तुतः पिता स्वस्थ नहीं थे। द्वारपाल उनका प्रणाम निवेदित करने के लिए भीतर नहीं जा रहा था। सम्भवतः उसे ऐसा ही आदेश दिया गया था। किन्तु, वह उन्हें भीतर जाने से रोक भी नहीं रहा था।
यदि पिता ने किसी के भी प्रवेश का निषेध किया है तो द्वारपाल का कर्तव्य है कि उन्हें भीतर जाने से रोके; और यदि पिता ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है तो उसे चाहिए कि भीतर जाकर उनका प्रणाम निवेदित करे....पर देवव्रत की तर्क-श्रृंखला यहीं रुक गयी। उन्हें लगा कि द्वारपाल के मन में भी कुछ स्पष्ट नहीं है। यहाँ सब कुछ अस्पष्ट है। ऐसी अस्पष्टता और द्वन्द्व की स्थिति में बेचारा द्वारपाल भी क्या करेगा-यही न कि न स्वयं भीतर जाने का साहस कर पायेगा और न उन्हें रोकने की धृष्टता....
‘‘राजवैध को सूचना दी गयी क्या ?’’
‘‘नहीं!’’
‘‘क्यों ?’’
सम्भवतः चक्रवर्ती का यही आदेश है।’’
देवव्रत कुछ सोचते हुए से खड़े रहे।
‘‘अमात्य कहाँ हैं ?’’ सहसा उन्होंने पूछा।
‘‘वे चक्रवर्ती के साथ यहाँ नहीं आये थे।’’
देवव्रत का माथा ठनकाः अमात्य क्यों नहीं आये ? वे पिता के साथ गये थे। वे अवश्य जानते होंगे कि पिता अस्वस्थ हैं। वे क्यों नहीं आये ? और राजवैद्य क्यों नहीं बुलाये गये ?....
अनुमान से ये सब कुछ नहीं जाना जा सकता । पिता से साक्षात्कार करना ही होगा।
देवव्रत ने कक्ष में प्रवेश किया।
पिता थके हुए-से, या असहाय रोगी के समान नहीं लौटे थे। वे अपने पलंग पर औधें मुँह पड़े थे। पहली दृष्टि में तो देवव्रत को लगा कि शायद पिता रो रहे हैं और स्वयं को सँभालने के प्रयत्न में ही बिस्तर पर औंधे हो गये हैं...देवव्रत के पग पृथ्वी पर चिपक गये। कितने कष्ट में हैं पिता। हस्तिनापुर के चक्रवर्ती, पुरुराज, वीरवर शान्तनु अपने कक्ष में अकेले पड़े
असहाय-से रो रहे हैं....मनुष्य कोई भी क्यों न हो-बलवान, ज्ञानी, चक्रवर्ती...आखिर मनुष्य है। शरीर और मन ने नियमों का दास। संसार के सुख-दुख से मुक्ति नहीं है उसकी। ...तो फिर जीवन में वह सुख-दुख मानता ही क्यों है ? वह जीवन को कार्य-कारण के नियमों के अधीन क्यों नहीं समझता ? जब यह सब अवश्यंभावी है तो इतने हाथ-पैर पटकने से क्या लाभ ? क्यों लपकता है मनुष्य लोभ और लाभ की ओर ? क्या पा जायेगा वह उसमें ? चक्रवर्ती शान्तनु स्वयं अपनी इच्छा से सुख पाने के लिए मृगया के लिए गये थे। क्या सुख मिला ? पड़े हुए आहत मृग के समान हाथ-पैर पटक रहे हैं कैसी पीड़ा है पिता को ? कहीं आखेट में कोई गहरा घाव तो नहीं खा गये ? पर नहीं। पिता शारीरिक घाव खाकर उसकी पीड़ा से रोनेवालों में से नहीं हैं। और यदि वैसा होता तो अमात्य साथ आये होते और इस समय यहाँ वैद्यों और शल्य चिकित्सकों का जमघट लगा होता.....
सहसा शान्तनु ने करवट बदली और जैसे अपनी किसी भीतरी पीड़ा से विविश होकर, उन्होंने अपने वक्ष पर दो-तीन घूँसे लगाये, मानो किसी उठते हुए आवेग को दबा रहे हों। उनका गहरा निःश्वास उनकी पीड़ा का भी प्रतीत था और उत्तेजना का भी। उन्होंने अपने समूचे शरीर को अकड़या और सारे संयम और नियन्त्रण के बावजूद अपनी दोनों टाँगें उठाकर पलंग पर पटक दीं। लगा वे अभी नियमित रूप से छटपटाते हुए हाथ-पैर पटकने लगेंगे।
तो पिता शीरीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं थे- देवव्रत ने सोचा-उनका मन उद्विग्न था। पर है तो उद्विग्नता भी रोग ही.....
‘‘पिताजी !’’ देवव्रत ने आगे बढ़, पिता के चरण छुए।
शान्तनु ने न उठकर पुत्र को गले से लगाया, न कोई आशीष दी। लोकाचार के अभ्यास की बाध्याता थी जैसे, अपनी हथेली देवव्रत के सिर पर रख दी।
देवव्रत ने देखा, पिता के चेहरे पर पीड़ा के तनाव की स्पष्ट रेखाएँ थीं। एक लम्बे प्रवास के बाद पुत्र को देखकर भी उनकी आँखों में वात्सल्य तो क्या एक हल्का-सा औपचारिक हास भी नहीं उतरा था। विचित्र भाव थे पिता की आकृति परः कभी ताप से दग्ध होते हुए निरीह जीव की पराजय कभी उग्र मानसिकता की दिग्दाह करने की व्यग्र हिंसा। दोनों में से एक भी भाव कुछ अधिक क्षणों तक टिक नहीं पाता था।....
देवव्रत को लगा, वे पिता से अपनी अवहेलना की शिकायत नहीं कर पायेंगे। इस प्रकार पीड़ा में तड़पना, मनुष्य दूसरों की भावना का क्या सम्मान कर पायेगा।..., फिर देवव्रत ने तो बहुत पहले ही स्वयं को समझा लिया था कि वे अपने पिता से .....पिता से क्या, किसी से भी कोमलता और स्नेह की कोई अपेक्षा नहीं करेंगे।
‘‘आप अस्वस्थ हैं पिताजी ?’’
शान्तनु ने एक क्षण के लिए स्थिर दृष्टि से पुत्र की ओर देखा और फिर जैसे सायास, अस्त-व्यस्त-से उठे खड़े हुए। अपने उत्तरीय को ठीक करने की व्यस्तता में इधर-उधर टलहते हुए, वे उत्तर को टालते रहे। देवव्रत के मन में जिज्ञासा जागीः थोड़ी-थोड़ी देर के लिए उभरनेवाला अपने प्रति उपालम्भ का वह हल्का-सा आभास....पर उपालम्भ का कारण ?
‘‘अस्वस्थ नहीं हूँ पुत्र !’’ शान्तनु अपना मन कुछ स्थिर करके बोले, ‘‘चिन्तित हूँ...चिन्ता से पीड़ित हूँ। चिन्ता की चिता का दाह सह रहा हूँ।’’ देवव्रत के मन में आया, कहें, ‘‘पिताजी ! आप उदभ्रान्त लगते हैं। आपका आचरण....।’’ पर देवव्रत ने कुछ कहा नहीं।
‘‘राजवैद्य को सूचना क्यों नहीं दी गयी पिताजी ?’’
‘‘कोई लाभ नहीं।’’
‘‘कारण जान सकता हूँ ?’’ देवव्रत का स्वर अत्यन्त विनीत था।
‘‘मुझे रोग नहीं, क्षोभ है। मेरी चिन्ता का समाधान वैद्य के पास नहीं है।’’
‘‘चक्रवर्ती सम्राटों को भी चिन्ताएँ होती हैं क्या?’’ देवव्रत को लगा, अपने मन से पूछा गया यह प्रश्न असावधानीवश उनके मुख से सशब्द निकल गया था। पर प्रश्न का दूसरा भाग उन्होंने अपने मन में ही रोक लिया था, ‘चिन्ताओं को दूर नहीं कर सकते तो ये सम्राज्य फिर किस काम के हैं ?’
शान्तनु ने पुत्र को नये सिरे से देखाः यह देवव्रत अनेक बार क्षत्रिय राजपुत्रों के समान नहीं, वनवासी वैरागियों के समान बातें करने लगता है। वनवासी ऋषियों के सान्निध्य में बिताया गया इसका आरम्भिक जीवन इसे राजपुत्रों की मानसिकता नहीं दे पाया है। शान्तनु को पहले इसका आभास हुआ तो वे पुत्र को आश्रमों में छोड़ने के स्थान पर, आचार्यों को ही राजमहल में बुला लेते।....न चाहते हुए भी वन वनवासियों के विरुद्ध उनका आक्रोश वाणी पा गया, ‘‘चक्रवर्ती सम्राटों को ही तो चिन्ताएँ होती हैं पुत्र ! कंगले वनवासियों के पास ऐसा होता ही क्या है, जिसकी वे चिन्ता करें।’’
‘‘अभाव की चिन्ता भी चिन्ता होती है पिताजी !’’ देवव्रत सहज भाव से बोले, ‘‘वरन् वह असुविधा भी होती है।’’
पर अधिकांश कथ्य, शब्दों के सहयोग के कारण उनके मन में ही रह गयाः यदि साम्राज्यों के साथ चिन्ताएँ ही जुड़ी हैं तो इतनी ललक से व्यक्ति साम्राज्य स्थापित करने के लिए लपकता ही क्यों है ? क्या मनुष्य इतनी-सी बात नहीं समझता कि उसका स्वार्थ किसमें है ? उसे किसका ग्रहण करना है, किसका त्याग ? यदि साम्राज्य चिन्ताओं का घर है तो मनुष्य को चाहिए कि उसे त्याज्य माने....
‘‘होगी ! ’’ शान्तनु ने उनकी बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वे अपनी चिन्ता में कहीं और गहरे उतर गये थे, ‘‘जाने क्यों गंगा ने मेरे सात पुत्रों को जीवन-मुक्त कर दिया....।
पिता जब भी इस घटना की ओर संकेत करते हैं, देवव्रत समझ नहीं पाते कि उनके मन में पत्नी की स्मृति जागी है या पुत्रों की। सात पुत्रों को जीवन-मुक्त करने वाले के लिए जो भाव पिता के मन में होना चाहिए था, उसका लेश मात्र भी शान्तनु के मन में नहीं था। कदाचित् उन सारी हृदय-विदारक घटनाओं के बाद भी आज तक उन्हें अपनी पत्नी के रूप की स्मृति मुग्ध करती थी। सन्तान को जीवन मुक्त करने वाली उस पत्नी से अब भी उन्हें वितृष्णा नहीं हुई थी। सन्तान भी उन्हें प्यारी रही होगी, तभी तो उन्होंने पत्नी को रुष्ट किया था; किन्तु सन्तान या पत्नी में से वे किसी एक को नहीं चाहते-दोनों को चाहते हैं। किन्तु यदि दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे वे ?....देवव्रत समझ नहीं पा रहे थे।
‘‘अब तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो।’’ शान्तनु पुनः बोले, ‘‘और मुझे बार-बार लगता है कि एक पुत्र का पिता, पुत्रहीन व्यक्ति से भी अधिक दुखी होता है।’’
‘‘क्यों पिताजी ?’’
‘‘पुत्र !’’ पहली बार शान्तनु का स्वर कुछ कोमल हुआ, ‘‘किसी मनुष्य के प्राण यदि एक निरीह और असहाय पक्षी में बन्द कर दिये जायें और पक्षी को स्वतन्त्र रूप से उड़ने के लिए मुक्त छोड़ दिया जाये तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी ?’’
देवव्रत ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पिता की बात पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
‘‘आकाश में गरुड़, श्येन तथा अन्य हिंस्र पक्षी हैं। धरती पर स्थान-स्थान पर बहेलिये के जाल बिछे हैं। किसी के लक्षित बाण या लक्ष्य-भ्रष्ट शस्त्र का वह निशाना हो सकता है।.... उस पक्षी की कोई हानि नहीं भी होती तो भी आशंकाओं के कारण उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, जिसके प्राण उसमें बन्द हैं; और यदि वह पक्षी मारा गया तो उस व्यक्ति का क्या होगा ?’’ शान्तनु ने जैसे उत्तर पाने के लिए देवव्रत की ओर देखा; और फिर स्वयं ही बोले, ‘‘तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो देवव्रत ! मेरे प्राण तुममें बसते हैं। तुम एक क्षण के लिए भी मुझसे विलग होते हो तो मेरी आत्मा व्याकुल हो उठती है....।
देवव्रत के मन में आया कि पिता का प्रतिवाद करें-यदि यह सच होता तो नगर-द्वार पर अगवानी के लिए आये खड़े पुत्र की अवहेलना कर पिता अपने महल में न आ गए होते। उसे स्वस्थ और प्रसन्न पाकर, उन्होंने उसे वहीं गले लगा लिया होता ...पुत्र इतना ही प्रिय था, तो उसे इस प्रकार नगर में अकेला छोड़कर नदियों के कछारों और बीहड़ वनों में मृगया का सुख पाने के लिए भटक न रहे होते।.... और अब, जब पुत्र सामने आया खड़ा है तो उसे उत्साहपूर्वक गले लगाकर सन्तोष प्रकट करने के स्थान पर, उद्विग्नता को गले लगाये न पड़े होते। पर देवव्रत ने यह सब कहा नहीं।
‘‘तुम शस्त्रधारी योद्धा हो पुत्र !’’ शान्तनु पहले की तुलना में कुछ आश्वस्त दिख रहे थे, ‘‘सदा युद्धों के लिए सन्नद्ध रहते हो। पर कुशल से कुशल योद्धा भी किसी-न-किसी दिन युद्ध में वीरगति पाता ही है। यदि किसी दिन तुम्हें वीरगति मिली तो मेरा क्या होगा पुत्र ? हस्तिनापुर के साम्राज्य का क्या होगा ? हमारे वंश का क्या होगा ? मेरी सद्गति कैसे होगी ?.....’’
देवव्रत के कान खड़े हो गये। क्या पिता विवाह का प्रस्ताव करनेवाले हैं ? क्या वंश-वृद्धि के नाम पर उनको घेरकर गृहस्थी की बेड़ियाँ पहनाना चाहते हैं। देवव्रत ने अपने शैशव में अपने माता-पिता के सम्बन्ध में, उनकी गृहस्थी के विषय में जो कुछ जाना और देखा-सुना है ...उसके बाद उनके मन में गृहस्थी के लिए कोई विशेष आकर्षण नहीं रह गया था।
अपनी माता और पिता की पीड़ा का लेशमात्र भी स्मरण होते ही, उनका मन इन सम्बन्धों से मुक्त होने के लिए पंख फड़फड़ाने लगता था। नारी का आकर्षण रूप भी देवव्रत के मन में कहीं वितृष्णा जगा जाता था...देवव्रत ने अपने भीतर कभी ऐसी रिक्ति का अनुभव नहीं किया, जिसे भरने के लिए उन्हें नारी के सान्निध्य की आवश्यकता हो। आज तक किसी नारी का रूप उसकी आँखों में नहीं उतरा, जो उसे रात भर जगाये रख सकता।...विवाह...अभी तो बार-बार उनका मन एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि व्यक्ति विवाह करता ही क्यों है ? शरीर सुख के लिए ? वंश-वृद्धि के लिए ? समाज और राष्ट्र के लिए ? किसके लिए है यह सारा हाहाकार ?......
‘‘गंगा के जाने के बाद मैंने दूसरा विवाह नहीं किया।’’ शान्तनु कह रहे थे, ‘‘आज भी नहीं करना चाहता। पर एक पुत्र....’’ उन्होंने रुककर देवव्रत को देखा, ‘‘जिसका पुत्र होता ही नहीं, उसे कुछ छिनने का भय नहीं होता, पर जिसका एक ही पुत्र हो, वह सदा उसके लिए...।
देवव्रत से पिता सहमत नहीं हो पा रहे थेः पिता को अपनी चिन्ता है या पुत्र की ? उनकी चिन्ता अपने लिए है या पुत्र के लिए ? उन्हें अपने पुत्र के लिए साम्राज्य चाहिए या अपने साम्राज्य के लिए पुत्र चाहिए ? अपना वंश वे क्यों चलाना चाहते हैं- अपनी सद्गति के लिए ?...पिता ने यह चिन्ता तो कभी नहीं की कि यदि उनका देहान्त हो गया तो उनके पुत्र का संरक्षक कौन होगा ? यदि राज्य नष्ट हो गया तो पुत्र के उपभोग के लिए सम्पत्ति कहाँ से आयेगी ?...
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i 






_m.jpg)