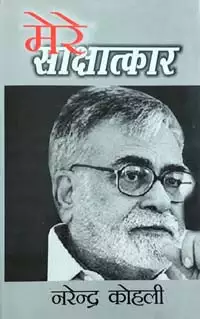|
बहुभागीय पुस्तकें >> महासमर - प्रच्छन्न महासमर - प्रच्छन्ननरेन्द्र कोहली
|
147 पाठक हैं |
|||||||
‘प्रच्छन्न’ महासमर का छठा खंड है। आप इसे पढ़ें और स्वयं अपने आप से पूछें– आपने इतिहास पढ़ा? पुराण पढ़ा? धर्मग्रंथ पढ़ा अथवा एक रोचक उपन्यास? इसे पढ़कर आपका मनोरंजन हुआ? आपका ज्ञान बढ़ा? अथवा आपका विकास हुआ? क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा कुछ पढ़ा था?
इस पुस्तक का सेट खरीदें।
Prachchann - The stories of Mahabharat by Narendra Kohli
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
महाकाल असंख्य वर्षों की यात्रा कर चुका है, किन्तु न मानव की प्रकृति परिवर्तित हुई है, न प्रकृति के नियम। उसका ऊपरी आवरण कितना भी भिन्न क्यों न दिखाई देता हो, मनुष्य का मनोविज्ञान आज भी वही है, जो सहस्त्रों वर्ष पूर्व था।
बाह्य संसार के सारे घटनात्मक संघर्ष वस्तुतः मन के सूक्ष्म विकारों के स्थूल रूपांतरण मात्र हैं। अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर जाए, तो ये मनोविकार, मानसिक विकृतियों में परणीत हो जाते हैं। दुर्योधन इसी प्रक्रिया का शिकार हुआ है। अपनी आवश्यकता भर पाकर वह संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरों का सर्वस्व छीनकर भी वह शांत नहीं हुआ। पांडवों की पीड़ा उसके सुख की अनिवार्य शर्त थी। इसलिए वंचित पांडवों को पीड़ित और अपमानित कर सुख प्राप्त करने की योजना बनाई गई। घायल पक्षी को तड़पाकर बच्चों को क्रीड़ा का-सा-आनन्द आता है। मिहिर कुल को अपने युद्धक गजों को पर्वत से खाई में गिरकर उनके पीड़ित चीत्कारों को सुनकर असाधारण सुख मिला था। अरब शेखों को ऊँटों की दौड़ में, उनकी पीठ पर बैठे बच्चों की अस्थियों और पीड़ा से चिल्लाने को देख-सुनकर सुख मिलता है। महासमर-6 में मनुष्य का मन अपने ऐसे ही प्रच्छन्न भाव उद्घाटित कर रहा है।
दुर्वासा ने बहुत तपस्या की है, किंतु न अपना अहंकार जीता है न क्रोध। एक अहंकारी और परपीड़क व्यक्तित्व, प्रच्छन्न रूप से उस तापस के भीतर विद्यमान है। वह किसी के द्वार पर आता है, तो धर्म देने के लिए नहीं। वह तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों को वरदान देने के लिए और सतोगुणी लोगों को वंचित करने के लिए आता है। पर पांडव पहचानते हैं कि संन्यासियों का समूह, जो उनके द्वार पर आया है सात्विक संन्यासियों का समूह नहीं है। यह एक प्रच्छन्न टिड्डी दल है जो उनके अन्न भण्डार को समाप्त करने आया है। ताकि जो पांडव दुर्योधन के शस्त्रों से न मारे जा सके, वे अपनी भूख से मर जाएँ।
दुर्योधन के सुख में प्रच्छन्न रूप से बैठा है, दुख और युधिष्ठिर की अव्यावहारिकता में प्रच्छन्न रूप से बैठा है धर्म। यह माया की सृष्टि है जो प्रकट रूप में दिखाई देता है, वह वस्तुतः होता नहीं, और जो वर्तमान है वह कहीं दिखाई नहीं देता।
पांडवों का आज्ञातवास, महाभारत-कथा का एक बहुत आकर्षक स्थल है। दुर्योधन की ग्रध्र दृष्टि से पांडव कैसे छिपे रह सके ? अपने आज्ञातवास के लिए पांडवों ने विराटनगर को ही क्यों चुना ? पांडवों के शत्रुओं में प्रच्छन्न मित्र कहां थे और मित्रों में प्रच्छन्न शत्रु कहाँ पनप रहे थे ?...ऐसे ही अनेक प्रश्नों को समेटकर आगे बढ़ती है, महासमर के इस छठे खंड ‘प्रच्छन्न की कथा। पाठक पूछता है कि यदि उसे महाभारत की ही कथा पढ़नी है तो वह व्यास कृत मूल महाभारत ही क्यों न पढ़े, नरेन्द्र कोहली का उपन्यास क्यों पढ़े ? वह यह भी पूछता है कि उसे उपन्यास ही पढ़ना है तो वह समसामायिक उपन्यास क्यों न पढ़े, नरेन्द्र कोहली का ‘महासमर’ ही क्यों पढ़े ??
‘महाभारत’ हमारा काव्य भी है, इतिहास भी और आध्यात्म भी। हमारे प्राचीन ग्रंथ शाश्वत सत्य की चर्चा करते हैं। वे किसी कालखंड के सीमित सत्य में आबद्ध नहीं हैं, जैसा कि यूरोपीय अथवा यूरोपीयकृत मस्तिष्क अपने अज्ञान अथवा बाहरी प्रभाव को मान बैठा है। नरेन्द्र कोहली ने न महाभारत को नए संदर्भों में लिखा है, न उसमें संशोधन करने का कोई दावा है। न वे पाठक को महाभारत समझाने के लिए उसकी व्याख्या मात्र कर रहे हैं। वे यह नहीं मानते कि महाकाल की यात्रा खंडों में विभाजित है, इसलिए जो घटनाएँ घटित हो चुकीं, उनसे अब हमारा कोई संबंध नहीं है। न तो प्रकृति के नियम बदले हैं, न मनुष्य का मनोविज्ञान। मनुष्य की अखंड कालयात्रा को इतिहास खंडों में बाँटे तो बाँटे, साहित्य उन्हें विभाजित नहीं करता, यद्यपि ऊपरी आवरण सदा ही बदलते रहते हैं।
महाभारत की कथा भारतीय चिंतन और भारतीय संस्कृति की अमूल्य थाती है। नरेन्द्र कोहली ने उसे ही अपने उपन्यास का आधार बनाया है। महासमर की कथा मनुष्य के उस अनवरत युद्ध की कथा है, जो उसे अपने बाहरी और भीतरी शत्रुओं के साथ निरंतर करना पड़ता है। वह उस संसार में रहता है, जिसमें चारों ओर लाभ और स्वार्थ की शक्तियाँ संघर्षरत हैं। बाहर से अधिक उसे अपने भीतर लड़ना पड़ता है। परायों से अधिक उसे अपनों से लड़ना पड़ता है। और वह अपने धर्म पर टिका रहता है तो वह इसी देह में स्वर्ग जा सकता है। इसका आश्वासन ‘महाभारत’ देता है। लोभ, त्रास और स्वार्थ के विरूद्ध धर्म के इस सात्विक युद्ध को नरेन्द्र कोहली एक आधुनिक और मौलिक उपन्यास के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।... और वह है ‘महासमर’। ‘प्रच्छन्न’ महासमर का छठा खंड है। आप इसे पढ़ें और स्वयं अपने आप से पूछें, आपने इतिहास पढ़ा ? पुराण पढ़ा ? धर्मग्रंथ पढ़ा अथवा एक रोचक उपन्यास ? इसे पढ़कर आपका मनोरंजन हुआ ? आपका ज्ञान बढ़ा ? अथवा आपका विकास हुआ ? क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा कुछ पढ़ा था ?
बाह्य संसार के सारे घटनात्मक संघर्ष वस्तुतः मन के सूक्ष्म विकारों के स्थूल रूपांतरण मात्र हैं। अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर जाए, तो ये मनोविकार, मानसिक विकृतियों में परणीत हो जाते हैं। दुर्योधन इसी प्रक्रिया का शिकार हुआ है। अपनी आवश्यकता भर पाकर वह संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरों का सर्वस्व छीनकर भी वह शांत नहीं हुआ। पांडवों की पीड़ा उसके सुख की अनिवार्य शर्त थी। इसलिए वंचित पांडवों को पीड़ित और अपमानित कर सुख प्राप्त करने की योजना बनाई गई। घायल पक्षी को तड़पाकर बच्चों को क्रीड़ा का-सा-आनन्द आता है। मिहिर कुल को अपने युद्धक गजों को पर्वत से खाई में गिरकर उनके पीड़ित चीत्कारों को सुनकर असाधारण सुख मिला था। अरब शेखों को ऊँटों की दौड़ में, उनकी पीठ पर बैठे बच्चों की अस्थियों और पीड़ा से चिल्लाने को देख-सुनकर सुख मिलता है। महासमर-6 में मनुष्य का मन अपने ऐसे ही प्रच्छन्न भाव उद्घाटित कर रहा है।
दुर्वासा ने बहुत तपस्या की है, किंतु न अपना अहंकार जीता है न क्रोध। एक अहंकारी और परपीड़क व्यक्तित्व, प्रच्छन्न रूप से उस तापस के भीतर विद्यमान है। वह किसी के द्वार पर आता है, तो धर्म देने के लिए नहीं। वह तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों को वरदान देने के लिए और सतोगुणी लोगों को वंचित करने के लिए आता है। पर पांडव पहचानते हैं कि संन्यासियों का समूह, जो उनके द्वार पर आया है सात्विक संन्यासियों का समूह नहीं है। यह एक प्रच्छन्न टिड्डी दल है जो उनके अन्न भण्डार को समाप्त करने आया है। ताकि जो पांडव दुर्योधन के शस्त्रों से न मारे जा सके, वे अपनी भूख से मर जाएँ।
दुर्योधन के सुख में प्रच्छन्न रूप से बैठा है, दुख और युधिष्ठिर की अव्यावहारिकता में प्रच्छन्न रूप से बैठा है धर्म। यह माया की सृष्टि है जो प्रकट रूप में दिखाई देता है, वह वस्तुतः होता नहीं, और जो वर्तमान है वह कहीं दिखाई नहीं देता।
पांडवों का आज्ञातवास, महाभारत-कथा का एक बहुत आकर्षक स्थल है। दुर्योधन की ग्रध्र दृष्टि से पांडव कैसे छिपे रह सके ? अपने आज्ञातवास के लिए पांडवों ने विराटनगर को ही क्यों चुना ? पांडवों के शत्रुओं में प्रच्छन्न मित्र कहां थे और मित्रों में प्रच्छन्न शत्रु कहाँ पनप रहे थे ?...ऐसे ही अनेक प्रश्नों को समेटकर आगे बढ़ती है, महासमर के इस छठे खंड ‘प्रच्छन्न की कथा। पाठक पूछता है कि यदि उसे महाभारत की ही कथा पढ़नी है तो वह व्यास कृत मूल महाभारत ही क्यों न पढ़े, नरेन्द्र कोहली का उपन्यास क्यों पढ़े ? वह यह भी पूछता है कि उसे उपन्यास ही पढ़ना है तो वह समसामायिक उपन्यास क्यों न पढ़े, नरेन्द्र कोहली का ‘महासमर’ ही क्यों पढ़े ??
‘महाभारत’ हमारा काव्य भी है, इतिहास भी और आध्यात्म भी। हमारे प्राचीन ग्रंथ शाश्वत सत्य की चर्चा करते हैं। वे किसी कालखंड के सीमित सत्य में आबद्ध नहीं हैं, जैसा कि यूरोपीय अथवा यूरोपीयकृत मस्तिष्क अपने अज्ञान अथवा बाहरी प्रभाव को मान बैठा है। नरेन्द्र कोहली ने न महाभारत को नए संदर्भों में लिखा है, न उसमें संशोधन करने का कोई दावा है। न वे पाठक को महाभारत समझाने के लिए उसकी व्याख्या मात्र कर रहे हैं। वे यह नहीं मानते कि महाकाल की यात्रा खंडों में विभाजित है, इसलिए जो घटनाएँ घटित हो चुकीं, उनसे अब हमारा कोई संबंध नहीं है। न तो प्रकृति के नियम बदले हैं, न मनुष्य का मनोविज्ञान। मनुष्य की अखंड कालयात्रा को इतिहास खंडों में बाँटे तो बाँटे, साहित्य उन्हें विभाजित नहीं करता, यद्यपि ऊपरी आवरण सदा ही बदलते रहते हैं।
महाभारत की कथा भारतीय चिंतन और भारतीय संस्कृति की अमूल्य थाती है। नरेन्द्र कोहली ने उसे ही अपने उपन्यास का आधार बनाया है। महासमर की कथा मनुष्य के उस अनवरत युद्ध की कथा है, जो उसे अपने बाहरी और भीतरी शत्रुओं के साथ निरंतर करना पड़ता है। वह उस संसार में रहता है, जिसमें चारों ओर लाभ और स्वार्थ की शक्तियाँ संघर्षरत हैं। बाहर से अधिक उसे अपने भीतर लड़ना पड़ता है। परायों से अधिक उसे अपनों से लड़ना पड़ता है। और वह अपने धर्म पर टिका रहता है तो वह इसी देह में स्वर्ग जा सकता है। इसका आश्वासन ‘महाभारत’ देता है। लोभ, त्रास और स्वार्थ के विरूद्ध धर्म के इस सात्विक युद्ध को नरेन्द्र कोहली एक आधुनिक और मौलिक उपन्यास के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।... और वह है ‘महासमर’। ‘प्रच्छन्न’ महासमर का छठा खंड है। आप इसे पढ़ें और स्वयं अपने आप से पूछें, आपने इतिहास पढ़ा ? पुराण पढ़ा ? धर्मग्रंथ पढ़ा अथवा एक रोचक उपन्यास ? इसे पढ़कर आपका मनोरंजन हुआ ? आपका ज्ञान बढ़ा ? अथवा आपका विकास हुआ ? क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा कुछ पढ़ा था ?
प्रकाशक
प्रच्छन्न
गांधारी ने स्वयं आग्रहपूर्वक अपने प्रासाद में निमंत्रित कर, शकुनि का ऐसा सत्कार किया था, जैसा राजप्रासादों में बहुत आत्मीय और सम्मानीय का अभ्यागतों का, अत्यंत असाधारण अवसरों पर ही किया जा सकता है। शकुनि को आदरपूर्वक मंच पर बैठने के पश्चात् उसने दो ही काम किए थेः विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट व्यंजन परोसने के लिए दासियों को आदेश दिए थे; तथा शकुनि से और भोजन करने का अनुरोधपूर्वक आग्रह किया था। शकुनि की समझ में नहीं आ रहा था कि आज गांधारी के मन में क्या था। किस प्रेरणा से आज उसके प्रासाद में, शकुनि का यह सम्मान सत्कार हो रहा था। गांधारी का व्यवहार सहज तो था; किंतु सामान्य नहीं था। शकुनि उसका सगा भाई था। उन्होंने सारा शैशव एक साथ व्यतीत किया था। उनका वंश एक था, उनका लक्ष्य एक था...फिर इस प्रकार आमंत्रित कर, साग्रह सत्कार करना....कोई तो प्रयोजन होना चाहिए। ....और गांधारी थी कि कुछ बोल ही नहीं रही थी।
शकुनि ने भोजन समाप्त कर हाथ धोए। वह सोच ही रहा था कि क्या अब उसे, गांधारी से सहज भाव से विदा माँग चुपचाप चला जाना चाहिए ? तभी गांधारी ने अपना मुख खोला, ‘‘भैया ! यहाँ, आकार बैठो, मेरे पास। तुमसे एक बात कहनी है।’’
शकुनि मन ही मन मुस्कायाः यह तो होना ही था। ऐसा भोजन कराकर गांधारी उसे यूँ ही चुपचाप कैसे विदा कर देती। वह तब से उसकी इसी बात की ही तो प्रतीक्षा कर रहा था। वह अपनी बहन को ठीक ही जानता था।
‘‘भैया !’’गांधारी बोली, ‘‘दुर्योधन मेरा पुत्र है।’’
शकुनि ने चकित दृष्टि से गांधारी की ओर देखाः क्या कहना चाहती है वह क्या शकुनि नहीं जानता कि दुर्योधन गांधारी का पुत्र है ? वह उसे इस प्रकार सूचना दे रही है, जैसे आज तक इस तथ्य से अनभिज्ञ रहा हो।
गांधारी की पट्टी बँधी आँखें नहीं देख सकती थीं कि शकुनि उसके चेहरे को ही एकटक देख रहा था; और उसकी आँखों में तनिक भी मधुर भाव नहीं था।
‘‘समझ रहे हो मेरी बात ? वह महाराज धृतराष्ट्र का ही पुत्र नहीं है। वह मेरा भी पुत्र है; और उससे मैं उतना ही प्रेम करती हूँ, जितना कोई माँ अपने पुत्र से कर सकती है।’’ गांधारी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, ‘‘अतः उसे अपना जीवनाश्व विनाश के मार्ग पर सरपट दौड़ाए लिए जाने की अनुमति नहीं दे सकती।’’
शकुनि कुछ नहीं बोला।
‘‘मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, ’’गांधारी पुनः बोली, ‘‘किंतु पता चला कि जब तक तुम उसे समझा रहे हो, तब तक वह किसी और के समझाने से कुछ नहीं समझेगा।’’
‘‘क्या समझाना चाहती हो उसे ?’’ शकुनि का मन जैसे स्तब्ध ही नहीं निस्पंद भी हो गया था। उसने गांधारी के मुँह से, इस प्रकार की बात सुनने की कभी कल्पना भी नहीं की थी।
‘‘वह आत्म-विकास और आत्म-विनाश का अंतर पहचाने। वह विनाश के मार्ग पर आगे न बढ़े।’’ गांधारी बोली।
‘‘तो इसमें समझाने को क्या रखा है ?’’ शकुनि बोला, ‘‘वह अपने शत्रुओं को उनकी धन-सम्पत्ति, सेना तथा सत्ता सबसे वंचित कर चुका है। बहुत संभव है, कि निकट भविष्य में वह उनका वध करने में भी सफल हो जाए। विनाश तो शत्रुओं का होगा गांधारी ! और शत्रुओं का संहार ही अपना उत्थान होता है। इसमें तुम्हें दुर्योधन का विनाश कहाँ से दिखाई पड़ रहा है ?’’
‘‘मैं तुमसे तर्क करना नहीं चाहती।’’ गांधारी ने कुछ कठोप स्वर में कहा, ‘‘केवल इतना कहना चाहती हूँ कि तुम दुर्योधन को उपलब्धियों की मृगतृष्णा में उलझाकर मृत्यु की ओर मत धकेलो। विकास के छदम मार्ग से उसे विनाश के मार्ग पर मत ले जाओ।’’
‘‘क्यों ? उपलब्धियों में क्या दोष है ? शकुनि का स्वर भी कुछ कठोर हो गया, ‘‘दुर्योधन के पास आज जो कुछ भी है वह सब मेरे ही कारण है। यदि मैंने उसे अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया, तो क्या अनुचित किया ? शत्रुओं का सर्वस्व हरण करने में यदि मैंने उसकी सहायता की तो उसका क्या अहित किया ? यदि मैंने उसे एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया, तो क्या मैंने उसका अकल्याण किया ?’’
‘‘नहीं ! इनमें विरोध नहीं है मेरा।’’ गांधारी बोली, ‘‘किंतु तुमने उसके मन में ईष्या की अग्नि जलाई, तुमने उसे धर्म के मार्ग से विरत किया, तुमने उसे नारी का अपमान करना सिखाया।....ये सारे मार्ग विनाश के द्वार तक ही जाते हैं। तुमने उसकी हीनतर वृत्तियों को प्रोत्साहित किया। उसे पशु बनाया। उसे उदात्ततर जीवन जीना नहीं सिखाया, वरन् उससे पूर्णतः विरत कर दिया।’’
शकुनि स्तब्ध रह गया। उसके मुख से जैसे अनायास ही निकल गया, ‘तो मुझसे और क्या अपेक्षा करती हो ?’’ और सहसा वह सँभल गया, ‘‘मैं कोई ऋषि नहीं हूँ। व्यास नहीं हूँ मैं ! मैं शकुनि हूँ। शकुनि कूटनीतिज्ञ है। कूटनीति सांसारिकता ही सिखाती है। भागिनेय को त्याग नहीं सिखा सकता मैं। कायरों के समान, अपना अधिकार शत्रुओं को सौंप, पलायन की शिक्षा नहीं दे सकता, मैं उसे।’’ वह कुछ रुककर पुनः बोला, ‘‘द्यूत में पांचाली को दाँव पर लगाने का प्रस्ताव अवश्य रखा था मैंने; किन्तु उसका अपमान करने जैसी कोई बात नहीं कही थी। उसे वेश्या कहने वाला वह धर्मात्मा कर्ण था, और पांचाली को निर्वस्त्र करने का आदेश देने का महाकार्य भी उसी ने किया था। उसे बुला कर समझा चुकीं क्या ?’’
गांधारी ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने जैसे अपनी ही बात आगे बढ़ाई, ‘‘मुझे लगता है भैया ! तुम्हारा सान्निध्य मेरे पुत्रों के लिए हितकर नहीं है। तुम उन्हें इतना महत्त्वाकांक्षी बना रहे हो कि वे धर्म-अधर्म को ही नहीं भूले, अपनी सुरक्षा-असुरक्षा को भी भूल गए हैं। तुमने उन्हें एक अंतहीन, अंधी भयंकर और वेगवती दौड़ में जोत दिया है, जो उसके वश की नहीं है। तुम देख रहे हो ये हाँफ रहे हैं, उनकी क्षमताएं क्षीण हो चुकी हैं। तुम जानते हो कि वे अधिक नहीं दौड़ पाएँगे; फिर भी तुम उन्हें दौड़ाते जा रहे हो। तुम चाहते हो कि वे दौड़ते-दौड़ते गिर पड़ें ? हाँफते-हाँफते अपने प्राण दे दें ?’’
शकुनि ने कुछ इस दृष्टि से गांधारी को देखा, जैसे संदेह हो रहा हो कि सामने बैठी यह स्त्री उसकी अपनी बहन ही थी, अथवा गांधारी के वेश में वहाँ कोई और आ बैठा था।
और सहसा उसका आक्रोश जागा, ‘‘जहाँ तक मैं समझता हूँ महारानी ! मैं अपने लक्ष्य से कण भर भी विचलित नहीं हुआ हूँ।’’
गांधारी मौन रही। उसकी आँखों पर पट्टी बँधी थी। शकुनि उसके आँखों के भाव नहीं देख सकता था; किंतु इतना तो समझ ही सकता था कि गांधारी का यह मौन, उसके लिए शुभ नहीं था।
अंततः गांधारी की आँखों में बंद भाव उसके चेहरे पर प्रकट हुआ। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया था। उसके शब्द अत्यंत कठोर थे, ‘‘तुम्हें मैं भली प्रकार जानती हूँ भैया ! तुम्हारी ही बहन हूँ।.....किंतु अब हस्तिनापुर की महारानी के रूप में आदेश दे रही हूँ। दुर्योधन को कामनाओं की सूली पर मत टाँगो; अन्यथा हस्तिनापुर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं होगा। जाओ। विवाद अथवा प्रतिवाद की अनुमति नहीं है तुम्हें। जाओ।’’
स्वयं को संयत रखने के लिए शकुनि को बहुत प्रयत्न करना पड़ा। गंधार में वह युवराज था। वह बड़ा भाई था, गांधारी उसकी छोटी बहन थी। उसकी आँखों में सीधे देख कर बात करने का साहस नहीं कर सकती थी वह। और आज वह उसे आदेश दे रही थी। हस्तिनापुर से निष्कासन की धमकी दे रही थी।.....किंतु क्या कर सकता था शकुनि ! सत्य यही था कि हस्तिनापुर में शकुनि कुरुओं का आश्रित था; और गांधारी हस्तिनापुर की महारानी थी इच्छा होने पर वह उसे वस्तुतः दंडित कर सकती थी। उसके आदेश से शकुनि हस्तिनापुर से निष्कासित भी हो सकता था।.....
शकुनि बिना एक भी शब्द कहे, उठ खड़ा हुआ। उसने एक दृष्टि गांधारी पर डाली; किंतु उसका लाभ क्या था गांधारी देख तो सकती नहीं थी कि शकुनि ने उसे किस दृष्टि से देखा था।....पहले सोचा कि इतना तो कह ही दे कि वह जा रहा है। फिर वह कहना भी आवश्यक नहीं लगा। उसकी पगध्वनि से वह दासी उसे बता ही देगी कि शकुनि चला गया।.....
अपने भवन में निजी कक्ष में पहुँचकर शकुनि ने कपाट भीतर से बंद कर लिए। उसे लग रहा था कि वह अपने कक्ष में ही नहीं, अपने मन में भी नितांत अकेला है....आज तक वह यही समझता रहा कि इस पराए राज्य में कोई और उसके साथ हो या न हो, उसकी बहन उसके साथ ही थी। वे दोनों बहन और –भाई एक ही लक्ष्य के लिए, संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे थे। उनका जीवन सामान ध्येय को समर्पित था। उनमें कहीं कोई भेद-भाव नहीं था।.....किंतु आज पता लगा था कि वह सब तो शकुनि को भ्रम ही था....
एक लम्बे समय तक उसे अपने इस एकाकीपन का कोई बोध नहीं था। कहाँ था यह एकाकीपन ? उसके अपने भीतर ही रहा होगा; किंतु कुडली मारे दम साधे पड़ा होगा। यहाँ तक की जिस शकुनि के भीतर यह छिपा बैठा था, उस शकुनि को ही उसके अस्तित्व का बोध नहीं था। आज ऐसा क्या हो गया था कि वह अपनी कुडंली त्याग, फन काढ़ कर खड़ा हो गया था, आकर उसे ही डराने लगा था....
वर्षों पहले, जब उसकी युवावस्था अपनी आँखें खोल ही रही थी इसी हस्तिनापुर के एक दूत के संदेश ने, गंधार के राजप्रसाद तथा राजवंश के हिला कर रख दिया था। कुरुकुल का भीष्म अपने नेत्रहीन भ्रातुष्पुत्र धृतराष्ट के लिए गांधार राजकुमारी का दान माँगा था। गांधार इतने शक्तिशाली नहीं थे कि हस्तिनापुर के शरीर के टुकड़े कर उसे बोरी में डाल, अश्व की पीठ से बाँध हस्तिनापुर लौटा देते; किंतु वे कुरुओं के इस आदेश को चुपचाप स्वीकार भी तो नहीं कर सकते थे।.....तब गांधारों ने ऐसे अवसरों के लिए, अपना परंपरागत मार्ग अपनाया था- धीरता का और धूर्तता का। शकुनि ने अपने जीवन के सारे स्वप्नों को छिन्न-भिन्न कर दिया था और कुरुओं द्वारा किए गए गांधारों के इस अपमान के प्रतिशोध को अपने जीवन का एक मात्र लक्ष्य मान, वह अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर चला आया था।....उसे यहीं रहना था। इन्हीं लोगों के मध्य। उसका अपना बन कर। उसे उसकी महत्त्वकांक्षाओं को जगाना था, उकसाना था,। महत्त्वपूर्ण आकांक्षाओं को नहीं, अपने व्यक्तिगत महत्त्व की आकांक्षाओं को जगाना था।....कितना सुविधापूर्ण था नेत्रहीन धृतराष्ट्र को समझाना कि राज्य तो वस्तुतः उसी का था किंतु उसे उससे वंचित कर दिया गया था; इसलिए उसे किसी भी प्रकार उसे प्राप्त करके ही दम लेना चाहिए।....शकुनि को सीधे धृतराष्ट्र को भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। वह तो गांधारी को ही स्मरण कराता रहता था। गांधारी का एक स्पर्श, धृतराष्ट्र को मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त था।.....और फिर यह भी लगा कि धृतराष्ट्र को कुछ सिखाने पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी।
उसके अपने ही भीतर इतना लोभ, मोह और स्वार्थ भरा हुआ था कि पूरे कुरुकुल को नष्ट करने के लिए, वह अकेला ही पर्याप्त था।.....वह तो कहो की भीष्म और विदुर उसके मन में जलनेवाली ज्वाला पर शीतल छींटे डालते रहते थे, अन्यथा वह अग्नि कब की, भरत वंश को जला चुकी होती।......शकुनि और गांधारी को इतना ही करना था कि वे धृतराष्ट्र को भीष्म और विदुर के धर्म से प्रभावित न होने देते।......
आज शकुनि स्मरण करने का प्रयत्न करता है, तो वह याद नहीं कर पाता कि उसका और गांधारी का मार्ग कब से पृथक हो गया; और उसे उसका आभास भी नहीं हुआ यह आभास तो आज ही हुआ, जब गांधारी ने उसे अपने कक्ष में बुलाकर कहा, ‘‘दुर्योधन मेरा पुत्र है भैया ! और मैं उससे प्रेम करती हूँ।’’ तो दुर्योधन अब भरत कुल का वंशज नहीं रहा,. जिसे नष्ट करने के लिए, शकुनि अपना प्रत्येक सुख छोड़ कर यहाँ आया था। वह गांधारी का पुत्र हो गया था। अब धृतराष्ट्र वह अत्याचारी राजा नहीं था, जिसने नेत्रहीन होते हुए भी, मात्र अपनी सैनिक शक्ति के बल पर, सुनयना गांधार राजकुमारी का अपरहण कर लिया था; और गांधारी ने उसका मुख देखना भी स्वीकार नहीं किया था। उसने अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली थी। आज धृतराष्ट्र गांधारी का मनभावन पति था।.... तो शकुनि ही मूर्ख था, जिसने आपना राज्य, राजधानी, कुल परिवार त्याग कर अपना सारा जीवन अपने कुल और अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए खपा डाला था।....आज गांधारी उसी वंश की रक्षा के लिए, अपने भाई को चेतावनी दे रही थी, जिसे नष्ट करने के लिए वे दोनों यहाँ आए थे।......
शकुनि यह क्यों नहीं समझ सका कि भाई बहन का एक परिवार तभी तक होता है, जब तक अपनी संतान नहीं हो जाती। वह तो आज तक यही मानता रहा कि उसका और गांधारी का एक ही परिवार है। उसने क्यों नहीं जाना कि इन संबंधों की प्रकृति बड़ी विचित्र है। मनुष्य की ममता अपने दाएँ-बाएँ खड़े बहन-भाईयों से तब तक ही होती है, जब तक उसको अपने सम्मुख खड़ी अपनी संतान दिखाई नहीं पड़ती। एक बार संतान हो जाए, तो बहन भाई साधन और माध्यम हो सकते हैं, ममता के पात्र नहीं रहते।
यदि गांधारी ने धृतराष्ट्र को अपना पति, कुरुकुल को अपना श्वसुर कुल तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया था। तो उसने उसी दिन शकुनि से क्यों नहीं कह दिया, ‘‘भैया ! अब अपने परिवार और अपने राज्य में लौट जाओ। जब मैंने इन परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है, तो तुम भी उन्हें स्वीकार कर लो।’’
आज जैसे शकुनि की आँखें खुल रही थीं.....क्यों कहती गांधारी यह सब उससे। अब वह कुरुकुल के विनाश की नहीं, धार्तराष्ट्रों कि विकास की इच्छुक थी। वह अपने पति के भी राजा बनाना चाहती थी और अपने पुत्र को भी।
....सकुनि ही मूर्ख था कि वह समझ नहीं सका कि कैसे अपने शत्रुओं के लिए उपयोगी हो गया था...आज गांधारी उसकी भर्त्सना कर रही है कि वह दुर्योधन को अधर्म के मार्ग पर ले जा रहा है।....अधर्म विनाश का मार्ग होता है; तो उस दिन क्यों नहीं बोली, पांडव को खांडव वन दिया गया था; उस दिन क्यों नहीं बोली, जब युधिष्ठिर को द्यूत के लिए हस्तिनापुर आने का आदेश दिया गया था ?
क्यों बोलती तब ? तब तो उसके पति और पुत्रों का अभ्युत्थान हो रहा था....अब, जब पांडवों का सर्वस्व हरण कर लिया गया था; दुर्योंधन सारे वैभव का स्वामी हो चुका था; उसकी स्थिति एक शक्तिशाली साम्राट् की सी हो गई थी.,.....अब यदि शकुनि को बीच से, दूध की मक्खी के समान निकालकर फेंक दिया जाए तो दुर्योधन का क्या बिगड़ेगा ?....अब गांधारी को अपने पुत्रों की सुरक्षा का ध्यान आ रहा था। अब उनके लिए शकुनि का सान्निध्य हानिकारक हो गया था।....
क्या गांधारी सचमुच इतनी चतुर राजनीतिज्ञ थी कि उसने शकुनि और अपने पुत्रों को तब तनिक भी नहीं टोका था जब तक शकुनि उन्हें उन्नति के मार्ग पर ले चल रहा था; और अब वह समझ गई कि आरोह का समय समाप्त हो चुका था, इसलिए शकुनि को बीच में से हटा दिया जाना चाहिए ? क्या वह जान गई थी कि उसके पुत्रों को अब शकुनि के माध्यम से कोई उपलब्धि नहीं होनेवाली ! अब शकुनि उन्हें उस मार्ग पर ले चलेगा, जिस पर चलने की तैयारी में उसने अपना सारा जीवन हस्तिनापुर में व्यातीत कर दिया था ?
तो शकुनि अब तो धार्तराष्ट्र के लिए अनावश्यक हो गया था ?....सच भी तो है, दुर्योधन, पांडवों से कुछ और छीनना चाहे, तो पांडवों के पास अब और है ही क्या ?...तो गांधारी ने ठीक ही पहचाना था कि पांडव अब और वंचित नहीं हो सकते थे। ऐसे में अब हस्तिनापुर में शकुनि की क्या आवश्यकता थी।......
शकुनि ने अपने मस्तक को एक झटका दिया। वह स्वयं को इस प्रकार प्रवंचित नहीं होने देगा। हस्तिनापुर में वह असहाय अवश्य है, किंतु इतना असहाय भी नहीं है कि अपना सारा यौवन नष्ट कर, मस्तक लटकाए चुपचाप गांधार लौट जाए।....गांधारी समझती है कि अब शकुनि की आवश्यकता नहीं है; किंतु दुर्योधन तो अभी ऐसा नहीं सोचता।......इससे पहले कि दुर्योधन भी कुछ ऐसा ही सोचने लगे, शकुनि को कुछ करना होगा। क्या कर सकता है जिसमें शकुनि दुर्योधन के सम्मुख अब वह कौन सा-ऐसा प्रलोभन रख सकता है, जिससे शकुनि दुर्योधन के लिए परम आवश्यक बना रहे ?...और यदि शकुनि दुर्योधन के लिए आवश्यक बना रहेगा, तो उस गांधारी का आदेश नहीं चल सकता। शायद गांधारी यह नहीं जानती थी कि हस्तिनापुर में आज्ञा ही नहीं, इच्छा भी दुर्योधन की ही चलती हैः राजा चाहे कोई भी हो, और महारानी चाहे गांधारी ही क्यों न हो।
और सकुनि के मन में एक योजना आकार ग्रहण करने लगी.,....विषधर का सा एक विचार उसके मन में निःशब्द रेंगा और फिर क्रमशः उसके अंग-प्रत्यंग स्पष्ट होने लगे। उस जीव की आँखें खुल कर चारों ओर देखने लगीं। फन तन कर सीधा हो गया और उसकी जिह्वा लपलपाने लगी।.....लोभ का अस्तित्व बाहर किसी भौतिक पदार्थ में होता है, अथवा मनुष्य के अपने मन में ?....मनुष्य का अहंकार अपनी उपालब्धियों से अधिक तृप्त होता है, अथवा अपने शतुत्रों की वंचना से ?....दुर्योधन के लिए अपना वैभव अधिक सुखद है अथवा युधिष्ठिर की अकिंचनता ? शत्रु को अभावों के कष्ट में तड़पते देखने में जो सुख है, वह अपनी बड़ी से बड़ी उपलब्धि में नहीं है।...ठीक है कि शकुनि अब दुर्योधन और कुछ भी नहीं उपलब्ध नहीं करवा सकता। किंतु वह उसे पांडवों की पीड़ा का सुख तो प्राप्त करवा ही सकता है।.....
शकुनि की दृष्टि में एक दृश्य जन्म ले रहा था.....एक बालक एक सर्प को ढेला मारता है। सर्प अपने घाव की पीड़ा से तड़पता है। बालक उसकी पीड़ा देख-देख कर प्रसन्न होता है। थोड़ी देर में सर्प अपनी पीड़ा से निढ़ाल हो कर अपना सिर टेक देता है। बालक की क्रीड़ा समाप्त हो जाती है। उसका सुख जैसे तिरोहित हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता। वह एक छड़ी लेकर सर्प को उकसाता है, उसे कोंचता है, उसके घावों को अपनी छड़ी से कुरेदता है छीलता है...और सर्प अपनी असह्य पीड़ा में भी अपना सिर उठा लेता है। बालक को फिर से क्रीड़ा का-सा सुख मिलने लगता है। वह सर्प को छड़ी से नहीं अपनी अँगुली से छेड़ता है। वह अपना हाथ उसके निकट ले जाता है। सर्प क्रोध में उसे दंश मारता है। अब तड़पने की बारी बालक की है....
बालक सर्प विष से पड़प-तड़प कर मर जाता है; और सर्प, सिर में लगे अपने घाव से।......
शकुनि मन ही मन मुस्कराया कुरुओं की रक्षा करना चाहती है। उन कुरुओं की जिन्होंने गांधारों का अपमान किया था। उस अपमान के प्रतिशोध का अवसर पाने के लिए शकुनि ने जीवन भर उनकी सेवा की। अब जब वह अवसर इतना निकट है, उनके सामने खड़ा है, तो गांधारी चाहती है कि वह चुपचाप गंधार लौट जाए।....वह भूल गई कि वह गांधारी है, गांधार राजकन्या। शायद अपने आपको कौरवी समझने लगी है।....
शकुनि की आँखों में एक कठोर भाव जन्मा।....यदि उसकी अपनी बहन गांधारी से कौरवी हो गयी तो उसे भी शकुनि की क्रोधाग्नि में जलना होगा
....शकुनि के लिए तो बस एक ही काम शेष रह गया है....दुर्योधन के हाथ में एक छड़ी पकड़ा देने भर का। वह स्वयं ही पांडवों को कोंचने के लिए द्वैत वन जा पहुँचेगा...और पांडवों को कोंचने का परिणाम....
शकुनि की इच्छा हुई कि वह जोर का एक अट्टाहास करे। इतने जोर का कि वह गांधारी के कानों में ही नहीं उसके मन में भी देर तक गूँजता रहे......
शकुनि ने भोजन समाप्त कर हाथ धोए। वह सोच ही रहा था कि क्या अब उसे, गांधारी से सहज भाव से विदा माँग चुपचाप चला जाना चाहिए ? तभी गांधारी ने अपना मुख खोला, ‘‘भैया ! यहाँ, आकार बैठो, मेरे पास। तुमसे एक बात कहनी है।’’
शकुनि मन ही मन मुस्कायाः यह तो होना ही था। ऐसा भोजन कराकर गांधारी उसे यूँ ही चुपचाप कैसे विदा कर देती। वह तब से उसकी इसी बात की ही तो प्रतीक्षा कर रहा था। वह अपनी बहन को ठीक ही जानता था।
‘‘भैया !’’गांधारी बोली, ‘‘दुर्योधन मेरा पुत्र है।’’
शकुनि ने चकित दृष्टि से गांधारी की ओर देखाः क्या कहना चाहती है वह क्या शकुनि नहीं जानता कि दुर्योधन गांधारी का पुत्र है ? वह उसे इस प्रकार सूचना दे रही है, जैसे आज तक इस तथ्य से अनभिज्ञ रहा हो।
गांधारी की पट्टी बँधी आँखें नहीं देख सकती थीं कि शकुनि उसके चेहरे को ही एकटक देख रहा था; और उसकी आँखों में तनिक भी मधुर भाव नहीं था।
‘‘समझ रहे हो मेरी बात ? वह महाराज धृतराष्ट्र का ही पुत्र नहीं है। वह मेरा भी पुत्र है; और उससे मैं उतना ही प्रेम करती हूँ, जितना कोई माँ अपने पुत्र से कर सकती है।’’ गांधारी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, ‘‘अतः उसे अपना जीवनाश्व विनाश के मार्ग पर सरपट दौड़ाए लिए जाने की अनुमति नहीं दे सकती।’’
शकुनि कुछ नहीं बोला।
‘‘मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, ’’गांधारी पुनः बोली, ‘‘किंतु पता चला कि जब तक तुम उसे समझा रहे हो, तब तक वह किसी और के समझाने से कुछ नहीं समझेगा।’’
‘‘क्या समझाना चाहती हो उसे ?’’ शकुनि का मन जैसे स्तब्ध ही नहीं निस्पंद भी हो गया था। उसने गांधारी के मुँह से, इस प्रकार की बात सुनने की कभी कल्पना भी नहीं की थी।
‘‘वह आत्म-विकास और आत्म-विनाश का अंतर पहचाने। वह विनाश के मार्ग पर आगे न बढ़े।’’ गांधारी बोली।
‘‘तो इसमें समझाने को क्या रखा है ?’’ शकुनि बोला, ‘‘वह अपने शत्रुओं को उनकी धन-सम्पत्ति, सेना तथा सत्ता सबसे वंचित कर चुका है। बहुत संभव है, कि निकट भविष्य में वह उनका वध करने में भी सफल हो जाए। विनाश तो शत्रुओं का होगा गांधारी ! और शत्रुओं का संहार ही अपना उत्थान होता है। इसमें तुम्हें दुर्योधन का विनाश कहाँ से दिखाई पड़ रहा है ?’’
‘‘मैं तुमसे तर्क करना नहीं चाहती।’’ गांधारी ने कुछ कठोप स्वर में कहा, ‘‘केवल इतना कहना चाहती हूँ कि तुम दुर्योधन को उपलब्धियों की मृगतृष्णा में उलझाकर मृत्यु की ओर मत धकेलो। विकास के छदम मार्ग से उसे विनाश के मार्ग पर मत ले जाओ।’’
‘‘क्यों ? उपलब्धियों में क्या दोष है ? शकुनि का स्वर भी कुछ कठोर हो गया, ‘‘दुर्योधन के पास आज जो कुछ भी है वह सब मेरे ही कारण है। यदि मैंने उसे अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया, तो क्या अनुचित किया ? शत्रुओं का सर्वस्व हरण करने में यदि मैंने उसकी सहायता की तो उसका क्या अहित किया ? यदि मैंने उसे एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया, तो क्या मैंने उसका अकल्याण किया ?’’
‘‘नहीं ! इनमें विरोध नहीं है मेरा।’’ गांधारी बोली, ‘‘किंतु तुमने उसके मन में ईष्या की अग्नि जलाई, तुमने उसे धर्म के मार्ग से विरत किया, तुमने उसे नारी का अपमान करना सिखाया।....ये सारे मार्ग विनाश के द्वार तक ही जाते हैं। तुमने उसकी हीनतर वृत्तियों को प्रोत्साहित किया। उसे पशु बनाया। उसे उदात्ततर जीवन जीना नहीं सिखाया, वरन् उससे पूर्णतः विरत कर दिया।’’
शकुनि स्तब्ध रह गया। उसके मुख से जैसे अनायास ही निकल गया, ‘तो मुझसे और क्या अपेक्षा करती हो ?’’ और सहसा वह सँभल गया, ‘‘मैं कोई ऋषि नहीं हूँ। व्यास नहीं हूँ मैं ! मैं शकुनि हूँ। शकुनि कूटनीतिज्ञ है। कूटनीति सांसारिकता ही सिखाती है। भागिनेय को त्याग नहीं सिखा सकता मैं। कायरों के समान, अपना अधिकार शत्रुओं को सौंप, पलायन की शिक्षा नहीं दे सकता, मैं उसे।’’ वह कुछ रुककर पुनः बोला, ‘‘द्यूत में पांचाली को दाँव पर लगाने का प्रस्ताव अवश्य रखा था मैंने; किन्तु उसका अपमान करने जैसी कोई बात नहीं कही थी। उसे वेश्या कहने वाला वह धर्मात्मा कर्ण था, और पांचाली को निर्वस्त्र करने का आदेश देने का महाकार्य भी उसी ने किया था। उसे बुला कर समझा चुकीं क्या ?’’
गांधारी ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने जैसे अपनी ही बात आगे बढ़ाई, ‘‘मुझे लगता है भैया ! तुम्हारा सान्निध्य मेरे पुत्रों के लिए हितकर नहीं है। तुम उन्हें इतना महत्त्वाकांक्षी बना रहे हो कि वे धर्म-अधर्म को ही नहीं भूले, अपनी सुरक्षा-असुरक्षा को भी भूल गए हैं। तुमने उन्हें एक अंतहीन, अंधी भयंकर और वेगवती दौड़ में जोत दिया है, जो उसके वश की नहीं है। तुम देख रहे हो ये हाँफ रहे हैं, उनकी क्षमताएं क्षीण हो चुकी हैं। तुम जानते हो कि वे अधिक नहीं दौड़ पाएँगे; फिर भी तुम उन्हें दौड़ाते जा रहे हो। तुम चाहते हो कि वे दौड़ते-दौड़ते गिर पड़ें ? हाँफते-हाँफते अपने प्राण दे दें ?’’
शकुनि ने कुछ इस दृष्टि से गांधारी को देखा, जैसे संदेह हो रहा हो कि सामने बैठी यह स्त्री उसकी अपनी बहन ही थी, अथवा गांधारी के वेश में वहाँ कोई और आ बैठा था।
और सहसा उसका आक्रोश जागा, ‘‘जहाँ तक मैं समझता हूँ महारानी ! मैं अपने लक्ष्य से कण भर भी विचलित नहीं हुआ हूँ।’’
गांधारी मौन रही। उसकी आँखों पर पट्टी बँधी थी। शकुनि उसके आँखों के भाव नहीं देख सकता था; किंतु इतना तो समझ ही सकता था कि गांधारी का यह मौन, उसके लिए शुभ नहीं था।
अंततः गांधारी की आँखों में बंद भाव उसके चेहरे पर प्रकट हुआ। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया था। उसके शब्द अत्यंत कठोर थे, ‘‘तुम्हें मैं भली प्रकार जानती हूँ भैया ! तुम्हारी ही बहन हूँ।.....किंतु अब हस्तिनापुर की महारानी के रूप में आदेश दे रही हूँ। दुर्योधन को कामनाओं की सूली पर मत टाँगो; अन्यथा हस्तिनापुर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं होगा। जाओ। विवाद अथवा प्रतिवाद की अनुमति नहीं है तुम्हें। जाओ।’’
स्वयं को संयत रखने के लिए शकुनि को बहुत प्रयत्न करना पड़ा। गंधार में वह युवराज था। वह बड़ा भाई था, गांधारी उसकी छोटी बहन थी। उसकी आँखों में सीधे देख कर बात करने का साहस नहीं कर सकती थी वह। और आज वह उसे आदेश दे रही थी। हस्तिनापुर से निष्कासन की धमकी दे रही थी।.....किंतु क्या कर सकता था शकुनि ! सत्य यही था कि हस्तिनापुर में शकुनि कुरुओं का आश्रित था; और गांधारी हस्तिनापुर की महारानी थी इच्छा होने पर वह उसे वस्तुतः दंडित कर सकती थी। उसके आदेश से शकुनि हस्तिनापुर से निष्कासित भी हो सकता था।.....
शकुनि बिना एक भी शब्द कहे, उठ खड़ा हुआ। उसने एक दृष्टि गांधारी पर डाली; किंतु उसका लाभ क्या था गांधारी देख तो सकती नहीं थी कि शकुनि ने उसे किस दृष्टि से देखा था।....पहले सोचा कि इतना तो कह ही दे कि वह जा रहा है। फिर वह कहना भी आवश्यक नहीं लगा। उसकी पगध्वनि से वह दासी उसे बता ही देगी कि शकुनि चला गया।.....
अपने भवन में निजी कक्ष में पहुँचकर शकुनि ने कपाट भीतर से बंद कर लिए। उसे लग रहा था कि वह अपने कक्ष में ही नहीं, अपने मन में भी नितांत अकेला है....आज तक वह यही समझता रहा कि इस पराए राज्य में कोई और उसके साथ हो या न हो, उसकी बहन उसके साथ ही थी। वे दोनों बहन और –भाई एक ही लक्ष्य के लिए, संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे थे। उनका जीवन सामान ध्येय को समर्पित था। उनमें कहीं कोई भेद-भाव नहीं था।.....किंतु आज पता लगा था कि वह सब तो शकुनि को भ्रम ही था....
एक लम्बे समय तक उसे अपने इस एकाकीपन का कोई बोध नहीं था। कहाँ था यह एकाकीपन ? उसके अपने भीतर ही रहा होगा; किंतु कुडली मारे दम साधे पड़ा होगा। यहाँ तक की जिस शकुनि के भीतर यह छिपा बैठा था, उस शकुनि को ही उसके अस्तित्व का बोध नहीं था। आज ऐसा क्या हो गया था कि वह अपनी कुडंली त्याग, फन काढ़ कर खड़ा हो गया था, आकर उसे ही डराने लगा था....
वर्षों पहले, जब उसकी युवावस्था अपनी आँखें खोल ही रही थी इसी हस्तिनापुर के एक दूत के संदेश ने, गंधार के राजप्रसाद तथा राजवंश के हिला कर रख दिया था। कुरुकुल का भीष्म अपने नेत्रहीन भ्रातुष्पुत्र धृतराष्ट के लिए गांधार राजकुमारी का दान माँगा था। गांधार इतने शक्तिशाली नहीं थे कि हस्तिनापुर के शरीर के टुकड़े कर उसे बोरी में डाल, अश्व की पीठ से बाँध हस्तिनापुर लौटा देते; किंतु वे कुरुओं के इस आदेश को चुपचाप स्वीकार भी तो नहीं कर सकते थे।.....तब गांधारों ने ऐसे अवसरों के लिए, अपना परंपरागत मार्ग अपनाया था- धीरता का और धूर्तता का। शकुनि ने अपने जीवन के सारे स्वप्नों को छिन्न-भिन्न कर दिया था और कुरुओं द्वारा किए गए गांधारों के इस अपमान के प्रतिशोध को अपने जीवन का एक मात्र लक्ष्य मान, वह अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर चला आया था।....उसे यहीं रहना था। इन्हीं लोगों के मध्य। उसका अपना बन कर। उसे उसकी महत्त्वकांक्षाओं को जगाना था, उकसाना था,। महत्त्वपूर्ण आकांक्षाओं को नहीं, अपने व्यक्तिगत महत्त्व की आकांक्षाओं को जगाना था।....कितना सुविधापूर्ण था नेत्रहीन धृतराष्ट्र को समझाना कि राज्य तो वस्तुतः उसी का था किंतु उसे उससे वंचित कर दिया गया था; इसलिए उसे किसी भी प्रकार उसे प्राप्त करके ही दम लेना चाहिए।....शकुनि को सीधे धृतराष्ट्र को भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। वह तो गांधारी को ही स्मरण कराता रहता था। गांधारी का एक स्पर्श, धृतराष्ट्र को मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त था।.....और फिर यह भी लगा कि धृतराष्ट्र को कुछ सिखाने पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी।
उसके अपने ही भीतर इतना लोभ, मोह और स्वार्थ भरा हुआ था कि पूरे कुरुकुल को नष्ट करने के लिए, वह अकेला ही पर्याप्त था।.....वह तो कहो की भीष्म और विदुर उसके मन में जलनेवाली ज्वाला पर शीतल छींटे डालते रहते थे, अन्यथा वह अग्नि कब की, भरत वंश को जला चुकी होती।......शकुनि और गांधारी को इतना ही करना था कि वे धृतराष्ट्र को भीष्म और विदुर के धर्म से प्रभावित न होने देते।......
आज शकुनि स्मरण करने का प्रयत्न करता है, तो वह याद नहीं कर पाता कि उसका और गांधारी का मार्ग कब से पृथक हो गया; और उसे उसका आभास भी नहीं हुआ यह आभास तो आज ही हुआ, जब गांधारी ने उसे अपने कक्ष में बुलाकर कहा, ‘‘दुर्योधन मेरा पुत्र है भैया ! और मैं उससे प्रेम करती हूँ।’’ तो दुर्योधन अब भरत कुल का वंशज नहीं रहा,. जिसे नष्ट करने के लिए, शकुनि अपना प्रत्येक सुख छोड़ कर यहाँ आया था। वह गांधारी का पुत्र हो गया था। अब धृतराष्ट्र वह अत्याचारी राजा नहीं था, जिसने नेत्रहीन होते हुए भी, मात्र अपनी सैनिक शक्ति के बल पर, सुनयना गांधार राजकुमारी का अपरहण कर लिया था; और गांधारी ने उसका मुख देखना भी स्वीकार नहीं किया था। उसने अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली थी। आज धृतराष्ट्र गांधारी का मनभावन पति था।.... तो शकुनि ही मूर्ख था, जिसने आपना राज्य, राजधानी, कुल परिवार त्याग कर अपना सारा जीवन अपने कुल और अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए खपा डाला था।....आज गांधारी उसी वंश की रक्षा के लिए, अपने भाई को चेतावनी दे रही थी, जिसे नष्ट करने के लिए वे दोनों यहाँ आए थे।......
शकुनि यह क्यों नहीं समझ सका कि भाई बहन का एक परिवार तभी तक होता है, जब तक अपनी संतान नहीं हो जाती। वह तो आज तक यही मानता रहा कि उसका और गांधारी का एक ही परिवार है। उसने क्यों नहीं जाना कि इन संबंधों की प्रकृति बड़ी विचित्र है। मनुष्य की ममता अपने दाएँ-बाएँ खड़े बहन-भाईयों से तब तक ही होती है, जब तक उसको अपने सम्मुख खड़ी अपनी संतान दिखाई नहीं पड़ती। एक बार संतान हो जाए, तो बहन भाई साधन और माध्यम हो सकते हैं, ममता के पात्र नहीं रहते।
यदि गांधारी ने धृतराष्ट्र को अपना पति, कुरुकुल को अपना श्वसुर कुल तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया था। तो उसने उसी दिन शकुनि से क्यों नहीं कह दिया, ‘‘भैया ! अब अपने परिवार और अपने राज्य में लौट जाओ। जब मैंने इन परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है, तो तुम भी उन्हें स्वीकार कर लो।’’
आज जैसे शकुनि की आँखें खुल रही थीं.....क्यों कहती गांधारी यह सब उससे। अब वह कुरुकुल के विनाश की नहीं, धार्तराष्ट्रों कि विकास की इच्छुक थी। वह अपने पति के भी राजा बनाना चाहती थी और अपने पुत्र को भी।
....सकुनि ही मूर्ख था कि वह समझ नहीं सका कि कैसे अपने शत्रुओं के लिए उपयोगी हो गया था...आज गांधारी उसकी भर्त्सना कर रही है कि वह दुर्योधन को अधर्म के मार्ग पर ले जा रहा है।....अधर्म विनाश का मार्ग होता है; तो उस दिन क्यों नहीं बोली, पांडव को खांडव वन दिया गया था; उस दिन क्यों नहीं बोली, जब युधिष्ठिर को द्यूत के लिए हस्तिनापुर आने का आदेश दिया गया था ?
क्यों बोलती तब ? तब तो उसके पति और पुत्रों का अभ्युत्थान हो रहा था....अब, जब पांडवों का सर्वस्व हरण कर लिया गया था; दुर्योंधन सारे वैभव का स्वामी हो चुका था; उसकी स्थिति एक शक्तिशाली साम्राट् की सी हो गई थी.,.....अब यदि शकुनि को बीच से, दूध की मक्खी के समान निकालकर फेंक दिया जाए तो दुर्योधन का क्या बिगड़ेगा ?....अब गांधारी को अपने पुत्रों की सुरक्षा का ध्यान आ रहा था। अब उनके लिए शकुनि का सान्निध्य हानिकारक हो गया था।....
क्या गांधारी सचमुच इतनी चतुर राजनीतिज्ञ थी कि उसने शकुनि और अपने पुत्रों को तब तनिक भी नहीं टोका था जब तक शकुनि उन्हें उन्नति के मार्ग पर ले चल रहा था; और अब वह समझ गई कि आरोह का समय समाप्त हो चुका था, इसलिए शकुनि को बीच में से हटा दिया जाना चाहिए ? क्या वह जान गई थी कि उसके पुत्रों को अब शकुनि के माध्यम से कोई उपलब्धि नहीं होनेवाली ! अब शकुनि उन्हें उस मार्ग पर ले चलेगा, जिस पर चलने की तैयारी में उसने अपना सारा जीवन हस्तिनापुर में व्यातीत कर दिया था ?
तो शकुनि अब तो धार्तराष्ट्र के लिए अनावश्यक हो गया था ?....सच भी तो है, दुर्योधन, पांडवों से कुछ और छीनना चाहे, तो पांडवों के पास अब और है ही क्या ?...तो गांधारी ने ठीक ही पहचाना था कि पांडव अब और वंचित नहीं हो सकते थे। ऐसे में अब हस्तिनापुर में शकुनि की क्या आवश्यकता थी।......
शकुनि ने अपने मस्तक को एक झटका दिया। वह स्वयं को इस प्रकार प्रवंचित नहीं होने देगा। हस्तिनापुर में वह असहाय अवश्य है, किंतु इतना असहाय भी नहीं है कि अपना सारा यौवन नष्ट कर, मस्तक लटकाए चुपचाप गांधार लौट जाए।....गांधारी समझती है कि अब शकुनि की आवश्यकता नहीं है; किंतु दुर्योधन तो अभी ऐसा नहीं सोचता।......इससे पहले कि दुर्योधन भी कुछ ऐसा ही सोचने लगे, शकुनि को कुछ करना होगा। क्या कर सकता है जिसमें शकुनि दुर्योधन के सम्मुख अब वह कौन सा-ऐसा प्रलोभन रख सकता है, जिससे शकुनि दुर्योधन के लिए परम आवश्यक बना रहे ?...और यदि शकुनि दुर्योधन के लिए आवश्यक बना रहेगा, तो उस गांधारी का आदेश नहीं चल सकता। शायद गांधारी यह नहीं जानती थी कि हस्तिनापुर में आज्ञा ही नहीं, इच्छा भी दुर्योधन की ही चलती हैः राजा चाहे कोई भी हो, और महारानी चाहे गांधारी ही क्यों न हो।
और सकुनि के मन में एक योजना आकार ग्रहण करने लगी.,....विषधर का सा एक विचार उसके मन में निःशब्द रेंगा और फिर क्रमशः उसके अंग-प्रत्यंग स्पष्ट होने लगे। उस जीव की आँखें खुल कर चारों ओर देखने लगीं। फन तन कर सीधा हो गया और उसकी जिह्वा लपलपाने लगी।.....लोभ का अस्तित्व बाहर किसी भौतिक पदार्थ में होता है, अथवा मनुष्य के अपने मन में ?....मनुष्य का अहंकार अपनी उपालब्धियों से अधिक तृप्त होता है, अथवा अपने शतुत्रों की वंचना से ?....दुर्योधन के लिए अपना वैभव अधिक सुखद है अथवा युधिष्ठिर की अकिंचनता ? शत्रु को अभावों के कष्ट में तड़पते देखने में जो सुख है, वह अपनी बड़ी से बड़ी उपलब्धि में नहीं है।...ठीक है कि शकुनि अब दुर्योधन और कुछ भी नहीं उपलब्ध नहीं करवा सकता। किंतु वह उसे पांडवों की पीड़ा का सुख तो प्राप्त करवा ही सकता है।.....
शकुनि की दृष्टि में एक दृश्य जन्म ले रहा था.....एक बालक एक सर्प को ढेला मारता है। सर्प अपने घाव की पीड़ा से तड़पता है। बालक उसकी पीड़ा देख-देख कर प्रसन्न होता है। थोड़ी देर में सर्प अपनी पीड़ा से निढ़ाल हो कर अपना सिर टेक देता है। बालक की क्रीड़ा समाप्त हो जाती है। उसका सुख जैसे तिरोहित हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता। वह एक छड़ी लेकर सर्प को उकसाता है, उसे कोंचता है, उसके घावों को अपनी छड़ी से कुरेदता है छीलता है...और सर्प अपनी असह्य पीड़ा में भी अपना सिर उठा लेता है। बालक को फिर से क्रीड़ा का-सा सुख मिलने लगता है। वह सर्प को छड़ी से नहीं अपनी अँगुली से छेड़ता है। वह अपना हाथ उसके निकट ले जाता है। सर्प क्रोध में उसे दंश मारता है। अब तड़पने की बारी बालक की है....
बालक सर्प विष से पड़प-तड़प कर मर जाता है; और सर्प, सिर में लगे अपने घाव से।......
शकुनि मन ही मन मुस्कराया कुरुओं की रक्षा करना चाहती है। उन कुरुओं की जिन्होंने गांधारों का अपमान किया था। उस अपमान के प्रतिशोध का अवसर पाने के लिए शकुनि ने जीवन भर उनकी सेवा की। अब जब वह अवसर इतना निकट है, उनके सामने खड़ा है, तो गांधारी चाहती है कि वह चुपचाप गंधार लौट जाए।....वह भूल गई कि वह गांधारी है, गांधार राजकन्या। शायद अपने आपको कौरवी समझने लगी है।....
शकुनि की आँखों में एक कठोर भाव जन्मा।....यदि उसकी अपनी बहन गांधारी से कौरवी हो गयी तो उसे भी शकुनि की क्रोधाग्नि में जलना होगा
....शकुनि के लिए तो बस एक ही काम शेष रह गया है....दुर्योधन के हाथ में एक छड़ी पकड़ा देने भर का। वह स्वयं ही पांडवों को कोंचने के लिए द्वैत वन जा पहुँचेगा...और पांडवों को कोंचने का परिणाम....
शकुनि की इच्छा हुई कि वह जोर का एक अट्टाहास करे। इतने जोर का कि वह गांधारी के कानों में ही नहीं उसके मन में भी देर तक गूँजता रहे......
;
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i