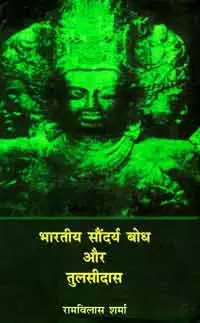|
लेख-निबंध >> परम्परा का मूल्यांकन परम्परा का मूल्यांकनरामविलास शर्मा
|
26 पाठक हैं |
|||||||
वस्तुतः इस कृति में, आधुनिक साहित्य के संदर्भ में, प्राचीन, मध्यकालीन और समकालीन भारतीय साहित्य का वर्णन हुआ है...
Prampara Ka Moolyakan
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रगतिशीलता के सन्दर्भ में परंपरा-बोध एक बुनियादी मूल्य है, फिर चाहे इस साहित्य के परिप्रेक्ष्य में रखा-परखा जाय अथवा समाज के। दूसरे शब्दों में बिना साहित्यक परंपरा को समझने न तो प्रगतिशील आलोचना और साहित्य की रचना हो सकती है और न ही अपनी ऐतिहासिक परंपरा से अलग रहकर कोई बड़ा सामाजिक बदलाव संभव है। लेकिन परंपरा में जो उपयोगी और सार्थक है, उसे उसका मूल्यांकन किए बिना नहीं अपनाया जा सकता है।
यह पुस्तक परंपरा के इसी उपयोगी और सार्थक की तलाश का प्रतिफलन है।
सुविख्यात समालोचक डॉ. रामविलास शर्मा ने जहाँ इसमें हिन्दी जाति के सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत की है, वहीं अपने-अपने युग में विशिष्ट भवभूति और तुलसी की लोकाभिमुख काव्य-चेतना का विस्तृत मूल्यांकन किया है। तुलसी के भक्तिकाव्य के सामाजिक मूल्यों का उद्घाटन करते हुए उनका कहना है कि दरिद्रता पर जितना अकेले तुलसीदास ने लिखा है उतना हिन्दी के समस्त नए-पुराने कवियों ने न मिलकर लिखा होगा। भवभूति के संदर्भ में रामविलासजी का यह निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण है कि यूनानी नाटककारों की देवसापेक्ष न्याय-व्यवस्था की जगह देवनिरपेक्ष न्याय-व्यवस्था का चित्रण शेक्सपियर से पहले भवभूति ने किया’ और रामायण-महाभारत के नाटकों के विषय में यह कि ‘राम और कृष्ण दोनों श्याम वर्ण के पुरुष हैं’।
वस्तुतः इस कृति में, आधुनिक साहित्य के जनवादी मूल्यों के संदर्भ में, प्राचीन, मध्यकालीन और समकालीन भारतीय साहित्य में अभिव्यक्त संघर्ष जनचेतना के उस विकासमान स्वरुप की पुष्टि हुई है जो शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों के प्रतिबिम्बित करता रहा है।
यह पुस्तक परंपरा के इसी उपयोगी और सार्थक की तलाश का प्रतिफलन है।
सुविख्यात समालोचक डॉ. रामविलास शर्मा ने जहाँ इसमें हिन्दी जाति के सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत की है, वहीं अपने-अपने युग में विशिष्ट भवभूति और तुलसी की लोकाभिमुख काव्य-चेतना का विस्तृत मूल्यांकन किया है। तुलसी के भक्तिकाव्य के सामाजिक मूल्यों का उद्घाटन करते हुए उनका कहना है कि दरिद्रता पर जितना अकेले तुलसीदास ने लिखा है उतना हिन्दी के समस्त नए-पुराने कवियों ने न मिलकर लिखा होगा। भवभूति के संदर्भ में रामविलासजी का यह निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण है कि यूनानी नाटककारों की देवसापेक्ष न्याय-व्यवस्था की जगह देवनिरपेक्ष न्याय-व्यवस्था का चित्रण शेक्सपियर से पहले भवभूति ने किया’ और रामायण-महाभारत के नाटकों के विषय में यह कि ‘राम और कृष्ण दोनों श्याम वर्ण के पुरुष हैं’।
वस्तुतः इस कृति में, आधुनिक साहित्य के जनवादी मूल्यों के संदर्भ में, प्राचीन, मध्यकालीन और समकालीन भारतीय साहित्य में अभिव्यक्त संघर्ष जनचेतना के उस विकासमान स्वरुप की पुष्टि हुई है जो शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों के प्रतिबिम्बित करता रहा है।
भूमिका
इस पुस्तक का विषय पहले निबन्ध से स्पष्ट हो जायेगा। साहित्य की परम्परा के मूल्याकन की समस्या आलोचना की महत्त्वपूर्ण समस्या है। मार्क्सवादी आलोचना के लिए वह विशेष रूप से महत्तवपूर्ण है। मार्क्स ने साम्यवाद के लिए कहा था कि वह ऐसा मानवतावाद है जो व्यक्तिगत सम्पत्ति के खात्मे से प्राप्त होता है। अपनी इस उक्ति से वह पुराने मानवतावाद और साम्यवाद का अन्तर बतलाते हैं। पुराना मानवतावाद उस व्यक्तिगत सम्पत्ति से अपने को सदा अलग नहीं रख पाता जिसके बल पर सम्पत्तिशाली वर्ग दूसरों का श्रमफल हथिया लेते हैं। किन्तु यदि पहले भी ऐसे साहित्यकार हुए हों जिनके पास व्यक्तित्व सम्पत्ति न रही हो तो उनका मानवातावाद मार्क्स के साम्यवाद के और भी निकट होगा। तुलसीदास कह गये हैं: लोक और धन है ही नहीं, इनका गर्व कैसे होगा ?
साम्यवादी संस्कृति समस्त मानव संस्कृति का अगला विकास है। यह विकास तभी सम्भव होगा जब संस्कृति का ज्ञान होगा। मानव संस्कृति का अर्थ है विभिन्न देशों की संस्कृति। इन देशों में भारत का स्थान महत्त्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति का सही ज्ञान तभी सम्भव है जब विश्व का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो। भारत में अनेक प्रदेश हैं, इन प्रदेशों की अलग-अलग भाषाएँ हैं, इन भाषाओं में रचा हुआ उनका अपना-अपना साहित्य है। हिन्दी साहित्य का महत्त्व समझने के लिए इन
प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य का थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक है। भारतीय साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन मेरी अन्य पुस्तक ‘भारतीय साहित्य का इतिहास’ में मिलेगा। (सम्भवता यह पुस्तक अगले वर्ष प्रकाशित हो जायेगी।) प्रस्तुत पुस्तक का सम्बन्ध हिन्दी-प्रदेश से है। इस साहित्य का मूल्याकन करते हुए जो अनेक निबन्ध मैंने समय-समय पर लिखे थे, वे यहां संकलित हैं पहले दो निबन्ध इस पुस्तक में पहली बार प्रकाशित हो रहे हैं। अन्य निबन्ध मेरे उन संग्रहों में आ चुके हैं जो पहली बार बहुत दिनों से अप्राप्य हैं। प्रेमचन्द वाले निबन्ध की सामग्री 1941 में प्रकाशित प्रेमचन्द पर मेरी पहली पुस्तक से ली गयी है। भाषा और साहित्य की परम्पराओं को अलग नहीं किया जा सकता। पुस्तक के कुछ निबन्धों में भाषा और भाषाशास्त्र की परम्परा का विश्लेषण है।
दीर्घ अवधि में लिखे हुए विभिन्न निबन्धों में एक-सा अपरिवर्तित दृष्टिकोण बना रहे, यह सम्भव नहीं है। अनुमान है कि मेरे दृष्टिकोण में कोई मौलिक परिवर्तन इन निबन्धों में न मिलेगा।
साम्यवादी संस्कृति समस्त मानव संस्कृति का अगला विकास है। यह विकास तभी सम्भव होगा जब संस्कृति का ज्ञान होगा। मानव संस्कृति का अर्थ है विभिन्न देशों की संस्कृति। इन देशों में भारत का स्थान महत्त्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति का सही ज्ञान तभी सम्भव है जब विश्व का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो। भारत में अनेक प्रदेश हैं, इन प्रदेशों की अलग-अलग भाषाएँ हैं, इन भाषाओं में रचा हुआ उनका अपना-अपना साहित्य है। हिन्दी साहित्य का महत्त्व समझने के लिए इन
प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य का थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक है। भारतीय साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन मेरी अन्य पुस्तक ‘भारतीय साहित्य का इतिहास’ में मिलेगा। (सम्भवता यह पुस्तक अगले वर्ष प्रकाशित हो जायेगी।) प्रस्तुत पुस्तक का सम्बन्ध हिन्दी-प्रदेश से है। इस साहित्य का मूल्याकन करते हुए जो अनेक निबन्ध मैंने समय-समय पर लिखे थे, वे यहां संकलित हैं पहले दो निबन्ध इस पुस्तक में पहली बार प्रकाशित हो रहे हैं। अन्य निबन्ध मेरे उन संग्रहों में आ चुके हैं जो पहली बार बहुत दिनों से अप्राप्य हैं। प्रेमचन्द वाले निबन्ध की सामग्री 1941 में प्रकाशित प्रेमचन्द पर मेरी पहली पुस्तक से ली गयी है। भाषा और साहित्य की परम्पराओं को अलग नहीं किया जा सकता। पुस्तक के कुछ निबन्धों में भाषा और भाषाशास्त्र की परम्परा का विश्लेषण है।
दीर्घ अवधि में लिखे हुए विभिन्न निबन्धों में एक-सा अपरिवर्तित दृष्टिकोण बना रहे, यह सम्भव नहीं है। अनुमान है कि मेरे दृष्टिकोण में कोई मौलिक परिवर्तन इन निबन्धों में न मिलेगा।
13 जनवरी 1981
रामविलास शर्मा
1
परम्परा का मूल्यांकन
जो लोग साहित्य में युग-परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रान्तिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए सीहित्य की परम्परा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषणमुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धान्तों को ऐतिहासित भोतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतिहास के ज्ञान के बिना ऐतिहासिक भौतिकता का ज्ञान सम्भव है ? कम से कम ऐतिहासिक भौतिकता के संस्थापकों की पुस्तकें पढ़ने से ऐसा नहीं लगता। जो महत्त्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परम्परा का है। इतिहास के ज्ञान से ही
ऐतिहासिक भौतिकवाद का विकास होता है, साहित्य की परम्परा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के ज्ञान से समाज में व्यापक परिवर्तन किये जा सकते हैं और नयी समाज-व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नये प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है ऐतिहासिक भौतिकवाद कुछ अमूर्त सिद्धान्तों का संग्रह नहीं है, वह मानव समाज के इतिहास का मूर्त ज्ञान है। वैसे ही प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धान्तों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परम्परा का मूर्त ज्ञान है। और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परम्परा।
ऐतिहासित भौतिकवाद के संस्थापकों के अनुसार जब से सभ्यता का विकास हुआ, व्यक्तिगत सम्पत्ति और वर्गों का अभ्युदय हुआ, तब सारी संस्कृति, समस्त साहित्य का विकास ऐसी समाज-व्यवस्था में हुआ है, जिसमें सम्पत्ति अधिकांश जनता के शोषण का साधन रही है। सामन्ती सम्पत्ति और पूँजीवादी व्यव्स्था में पूँजीवादी सम्पत्ति अपने साथ के तमाम आर्थिक सम्बन्धों सहित शोषण-व्यवस्था कायम किये रही है। सभ्य समाज में सदैव सम्पत्ति- शाली वर्गों का प्रभुत्व रहा है। अब जिस नये समाज की रचना करनी है, उसमें इस प्रभुत्व को समाप्त कर दिया जायेगा; जिस नयी सभ्यता की रचना करनी है, वह पुरानी सभ्यता से गुणात्म रूप से भिन्न होगी। तब पुराने इतिहास की ज़रूरत क्या है ? नयी सभ्यता को पुरानी सभ्यता की ज़रूरत क्या है ?
नयी सभ्यता पुरानी सभ्यता से गुणात्मक रूप से भिन्न होगी, ऐतिहासिक प्रक्रिया का यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि वह पुरानी सभ्यता की समस्त उपलब्धियों को आत्मसात् करके आगे बढ़ेगी और इतने बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें अपनायेगी कि वैसा कार्य मानव इतिहास में अभूतपूर्व होगा।
मनुष्य जाति का इतिहास- आदिम गण समाजों के विघटन के बाद-वर्ग-संघर्ष का इतिहास है। जब-जब शोषित वर्गों ने अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष किया, तब-तब उनका यह संघर्ष उनके उत्तराधिकारी नये समाज के विधायकों के लिए महत्त्वपूर्ण रहा है। इसके साथ उन्होंने अपने वर्ग हितों के अनुकूल अपनी संस्कृति, अपने साहित्य की रचना की है। पर इसके अलावा सभ्यता का इतिहास वर्ग-सहयोग का इतिहास भी है। भले ही यह सहयोग
शोषक वर्ग के लोगों को फुसलाकर, डरा-धमकाकर या दबाकर प्राप्त किया हो, बलप्रयोग द्वारा उन्हें अपनी आज्ञा मानने पर बाध्य किया हो, पर है वह वर्ग-सहयोग। प्रश्न¬ इच्छा-अनिच्छा का नहीं है, प्रश्न ऐतिहासिक प्रक्रिया के वस्तुगत रूप का है। सैकड़ों पीढ़ियों तक श्रमिक जनता ने जिस सभ्यता का निर्माण किया है, जो उसके श्रम के बिना अस्तित्व ही में न आती, क्या उनके प्रति उनका नकारात्मक रुख अपनाना सही है ? अनेक देशों में ऐसा हुआ है कि सामन्ती व्यवस्था खत्म करने के बाद जनता ने राजप्रासादों का उपयोग अपने हित में किया। उसने उसकी पहले से और भी अधिक रक्षा की और पहले की अपेक्षा उनका और भी अच्छा उपयोग किया। तब पुरानी संस्कृति के कौन से तत्त्व श्रमिक जनता के काम आ सकते हैं, कौन से तत्त्व उसके लिए हानिकारक हैं, इसका निर्धारण आवश्यक होता है।
ऐतिहासिक विकासक्रम में किसी भी समाज व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पत्तिशाली वर्ग की भूमिका उस व्यवस्था के अभ्युदय काल में यह सम्पत्तिशाली वर्ग पुरानी व्यवस्था को बदलता है और सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अपने ह्रास काल में वह अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है, सामाजिक परिवर्तन के आड़े आता है, सभ्यता के विकास में बाधक बनता है दोनों स्थितियों में वह जिस तरह की संस्कृति को प्रश्रय देता है, उसमें बहुत बड़ा अन्तर है।
इसलिए साहित्य की परम्परा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिम्बित कराता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहां तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे सम्पत्तिशाली वर्गों की
देख-रेख में रचा है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिम्बित करता है, उसे भी परखकर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का। यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूप-रेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। जहाँ पूँजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया है, वहीं यह सम्भावना होती है कि सम्पत्तिशाली और सम्पत्ति हीन वर्ग एक-दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हों। पुराने साहित्य में वर्ग-हित साफ़-साफ़- टकराते हुए दिखाई दें, इसकी सम्भावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्त्वों की तरह साहित्य में ऐसे तत्त्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम में
आते हैं। आग की तरह जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्त्व बन गया है। कल-कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होती है और पूँजीवादी व्यवस्था में भी। सभ्यता का हर स्तर वर्गबद्ध नहीं होता। इसी तरह साहित्य का हर स्तर सम्पक्तिशाली वर्गों के हितों से बँधा हुआ नहीं रहता। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना क्योंकि इसका अविष्कार पूँजीवादी समाज में हुआ था। और उसका उपयोग भी पूँजीपतियों ने अपने हित में किया था।
साहित्य मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन से सम्बद्ध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत-सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणिमात्र से जोड़ती हैं। इस बात को बार-बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। उसमें मनुष्य का इन्द्रिय-बोध, उसकी भावनाएँ आन्तरिक प्रेरणाएँ भी व्यंजित होती हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है।
जिस समय ऐतिहासिक भौतिकता की स्थापना हुई, उस समय जीव-विज्ञान में विकासवाद का बोलबाला था। यह विकासवाद सही हो चाहे गलत, यह बात सच है कि साहित्य में विकास-प्रक्रिया उसी तरह सम्पन्न नहीं होती जैसे समाज में। सामाजिक विकास-क्रम में सामन्ती सभ्यता की अपेक्षा पूँजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है और पूँजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को। पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गयी है। पर यह आवश्यक नहीं है कि सामन्ती समाज के कवि की अपेक्षा पूँजीवादी समाज का
कवि श्रेष्ठ हो। यह भी सम्भव है कि आधुनिक सभ्यता विकास कविता का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा हो। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि-क्या भारत में और क्या यूरुप में –पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं और कहीं उनके आस-पास पहुँच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, वे उनका अनुकरण नहीं करते उससे सीखते हैं, और स्वयं नयी परम्पराओं को जन्म देते हैं। और जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए, वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृति असमर्थता का
सूचक होता है। जो महान साहित्यकार हैं, उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा को अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौन्दर्य ज्यों-का-त्यों नहीं रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अन्तर है। अमरीका ने ऐटमबम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज़ का उत्पादन दुबारा इग्लैंड में भी नहीं हुआ।
भौतिकवाद दो तरह का है, एक यान्त्रिक भौतिकवाद, दूसरा द्धन्द्धात्मक भौतिवाद। यान्त्रिक भौतिकवाद की की विशेषता यह है कि वह चेतना को आर्थिक सम्बन्धों का प्रतिबिम्ब मात्र मानता है। प्रतिबिम्ब यान्त्रिक होता ही है। जब चेतना प्रतिबिम्ब है, तब संस्कृति का ताना-बाना भी पूरी तरह बदल जाता है। इस यान्त्रिक भौतिकवाद का विकास फ्रान्स में हुआ; 19वीं सदी में जब भौतिक विज्ञान का विकास हुआ, तो इस विज्ञान का दार्शनिक दृष्टिकोण इसी यान्त्रिक
भौतिकवाद से प्रभावित हुआ। इसके विपरीत द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक सम्बन्धों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक सम्बन्धों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकता का अर्थ भाग्य-बाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं हो जाता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं हैं। दोनों का सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्षरूप में स्वाधीन होता है।
गुलामी अमरीका में थी और गुलामी एथेन्स में थी किन्तु एथेन्स की सभ्यता ने सारे यूरुप को प्रभावित किया और गुलामों के अमरीकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामन्तवाद दुनिया भर में कायम रहा। पर इस सामन्ती दुनिया में महान् कविता के दो ही केन्द्र थे- भारत और ईरान। पूँजीवादी विकास यूरुप के तमाम देशों में हुआ पर रैफेल, लेओनार्दों दा विंची और माइकेल ऐंजेलो इटली की देन हैं। यहां हम एक ओर यह देखते हैं कि विशेष सामाजिक
परिस्थितियों में कला का विकास सम्भव होता है, दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियाँ होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। जिस तरह औद्योगिक उत्पादन का समाजीकरण पूँजीवादी व्यवस्था में होता हैं, उस तरह साहित्यिक रचना का समाजिकरण नहीं होता। कारखाने में 1500 मज़दूर मिलकर दिन-प्रतिदिन थान के थान कपड़े निकाल सकते है। यदि साहित्यकारों को साहित्य-रचना के कारखाने में भर्ती कर दिया जाए तो हो सकता है कि उनके कुछ दोष दूर हो जायें, अथवा वे एक दूसरे से इतना लड़ें कि और किसी काम के लिए उन्हें फुरसत न मिले, पर नियमित रूप से उच्च कोटि के
उपन्यास, काव्य, नाटक के लिए उन्हें फुरसत न मिले, पर नियमित रूप से उच्च कोटि के उपन्यास, काव्य, नाटक, पंचवर्षीय योजना के अनुसार, उस कारखाने से निकलते रहेंगे, इसकी सम्भावना ज़रा कम है। साहित्यकार आपसी सहयोग से लाभ उठाते हैं पर अभी उस तकनीक का पता नहीं लगाया जा सका जिसे लोगों को सिखाकर साहित्य का सामूहिक उत्पादन किया जा सके।
साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। इसका यह अर्थ नहीं कि ये मनुष्य जो कुछ करते हैं। वह सब अच्छा ही अच्छा होता है, या उनके श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होते है। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। ऐसी कला निर्जीव होती है। इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफी निन्दा की जाती है। किन्तु जो लोग सबसे ज्यादा व्यक्ति-पूजा की निन्दा करते हैं, वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति-पूजा का प्रचार भी करते हैं। अन्तर इतना होता है कि ब्रह्मा की जगह उन्होंने विष्णु को बिठा दिया। लेकिन पूजा तो पूजा। ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यदि कोई भी
साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है, तो राजनीतिज्ञ यह दावा और भी नहीं कर सकते, इसलिए कि साहित्य के मूल्य, राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा, अधिक स्थायी हैं। अंग्रेज कवि टेनीसन ने लैटिन कवि वर्जिल कर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया। पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि-तरंगें हमें आज भी सुनायी देती हैं और हृदय को आनन्द-विह्यल कर देती हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानीदेवा v रह जायेगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शेली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नज़र आयेंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की उपेक्षा करोड़ों नयी आँखें देखेंगी।
साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह, जनसमुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि पुरुष के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है, वह अन्य किसी जाति की नहीं है। जनसमुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। प्राचीन यूनान अनेक गणसमाजों में बँटा हुआ था। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी
एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं ? 19वीं सदी में शेली और बायरन अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसी एकात्मकता पहचानने में बड़ा परिश्रम किया। भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि वह विच्छिन्न है और अविच्छिन्न भी। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्त्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परम्परा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
बंगाल विभाजित हुआ और है, किन्तु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परम्परा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए, तो ज्ञात हो जायेगा कि साहित्य की परम्परा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं।
एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएँ बोलनेवाले राष्ट्र की भी अस्मित होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं, अनेक भाषा-भाषी हैं। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्त्वों पर मुसीबत आती है, तब उन्हें अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान होता बहुत अच्छी तरह हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। सोवियत संघ के लोग हिटलर-विरोधी संग्राम को उचित ही महान् राष्ट्रीय (अथवा देशभक्तिपूर्ण) संग्राम कहते हैं। इस युद्ध के दौरान खासतौर से रूसी जाति ने
बार-बार अपनी साहित्य-परम्परा का स्मरण किया। सोवियत समाज ज़ारशाही रुस के समाज से भिन्न है। समाज-व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रवाह अविच्छन्न है। ज़ारशाही रूस जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान् साहित्यकार हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खण्डित नहीं होती वरन् और पुष्ट होती है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ है और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है जैसी वह 1917 से पहले नहीं थी। ज़ारशाही रूस में बहुत-सी जातियाँ पराधीन
बनाकर रखी गयी थीं। उन सब पर रूसी जाति के सामन्त और पूँजीपति शासन करते थे। जैसे और बहुत-से साम्राज्य होते हैं, वैसे ही यह भी साम्राज्य था। 1917 की क्रान्ति के बाद रूसी और गैररूसी जातियों के आपसी सम्बन्धों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत-सी जातियाँ सोवियत संघ में शामिल न हुईं, अलग हो गयीं। कुछ विलम्ब से, दूसरे महायुद्द से कुछ ही पहले, अन्य जातियाँ उसमें सामिल हुईं। सोवियत संघ में आज जितनी जातियाँ शामिल हैं, उनका वैसा मिला-जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है, जैसा भारत की जातियों का है। राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रवाह बहुत बड़ी
निर्धारक शक्ति है। यूरुप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं। पर यूरुप कभी राष्ट्र नहीं बना। और अब तो पूर्वी यूरुप और पश्चिमी यूरुप, दो यूरुप का अलग उल्लेख आम बात है। संसार का कोई भी देश, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से, इतिहास को ध्यान में रखें तो, भारत का मुकाबला नहीं कर सकता।
यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई। वह मुख्यतः संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति में रामायण और महाभारत को अलग कर दें, तो भारतीय साहित्य की आन्तरिक एकता टूट जायेगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही, जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकी की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परम्परा का मूल्यांकन उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है।
ऐतिहासिक भौतिकवाद का विकास होता है, साहित्य की परम्परा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के ज्ञान से समाज में व्यापक परिवर्तन किये जा सकते हैं और नयी समाज-व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नये प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है ऐतिहासिक भौतिकवाद कुछ अमूर्त सिद्धान्तों का संग्रह नहीं है, वह मानव समाज के इतिहास का मूर्त ज्ञान है। वैसे ही प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धान्तों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परम्परा का मूर्त ज्ञान है। और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परम्परा।
ऐतिहासित भौतिकवाद के संस्थापकों के अनुसार जब से सभ्यता का विकास हुआ, व्यक्तिगत सम्पत्ति और वर्गों का अभ्युदय हुआ, तब सारी संस्कृति, समस्त साहित्य का विकास ऐसी समाज-व्यवस्था में हुआ है, जिसमें सम्पत्ति अधिकांश जनता के शोषण का साधन रही है। सामन्ती सम्पत्ति और पूँजीवादी व्यव्स्था में पूँजीवादी सम्पत्ति अपने साथ के तमाम आर्थिक सम्बन्धों सहित शोषण-व्यवस्था कायम किये रही है। सभ्य समाज में सदैव सम्पत्ति- शाली वर्गों का प्रभुत्व रहा है। अब जिस नये समाज की रचना करनी है, उसमें इस प्रभुत्व को समाप्त कर दिया जायेगा; जिस नयी सभ्यता की रचना करनी है, वह पुरानी सभ्यता से गुणात्म रूप से भिन्न होगी। तब पुराने इतिहास की ज़रूरत क्या है ? नयी सभ्यता को पुरानी सभ्यता की ज़रूरत क्या है ?
नयी सभ्यता पुरानी सभ्यता से गुणात्मक रूप से भिन्न होगी, ऐतिहासिक प्रक्रिया का यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि वह पुरानी सभ्यता की समस्त उपलब्धियों को आत्मसात् करके आगे बढ़ेगी और इतने बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें अपनायेगी कि वैसा कार्य मानव इतिहास में अभूतपूर्व होगा।
मनुष्य जाति का इतिहास- आदिम गण समाजों के विघटन के बाद-वर्ग-संघर्ष का इतिहास है। जब-जब शोषित वर्गों ने अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष किया, तब-तब उनका यह संघर्ष उनके उत्तराधिकारी नये समाज के विधायकों के लिए महत्त्वपूर्ण रहा है। इसके साथ उन्होंने अपने वर्ग हितों के अनुकूल अपनी संस्कृति, अपने साहित्य की रचना की है। पर इसके अलावा सभ्यता का इतिहास वर्ग-सहयोग का इतिहास भी है। भले ही यह सहयोग
शोषक वर्ग के लोगों को फुसलाकर, डरा-धमकाकर या दबाकर प्राप्त किया हो, बलप्रयोग द्वारा उन्हें अपनी आज्ञा मानने पर बाध्य किया हो, पर है वह वर्ग-सहयोग। प्रश्न¬ इच्छा-अनिच्छा का नहीं है, प्रश्न ऐतिहासिक प्रक्रिया के वस्तुगत रूप का है। सैकड़ों पीढ़ियों तक श्रमिक जनता ने जिस सभ्यता का निर्माण किया है, जो उसके श्रम के बिना अस्तित्व ही में न आती, क्या उनके प्रति उनका नकारात्मक रुख अपनाना सही है ? अनेक देशों में ऐसा हुआ है कि सामन्ती व्यवस्था खत्म करने के बाद जनता ने राजप्रासादों का उपयोग अपने हित में किया। उसने उसकी पहले से और भी अधिक रक्षा की और पहले की अपेक्षा उनका और भी अच्छा उपयोग किया। तब पुरानी संस्कृति के कौन से तत्त्व श्रमिक जनता के काम आ सकते हैं, कौन से तत्त्व उसके लिए हानिकारक हैं, इसका निर्धारण आवश्यक होता है।
ऐतिहासिक विकासक्रम में किसी भी समाज व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पत्तिशाली वर्ग की भूमिका उस व्यवस्था के अभ्युदय काल में यह सम्पत्तिशाली वर्ग पुरानी व्यवस्था को बदलता है और सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अपने ह्रास काल में वह अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है, सामाजिक परिवर्तन के आड़े आता है, सभ्यता के विकास में बाधक बनता है दोनों स्थितियों में वह जिस तरह की संस्कृति को प्रश्रय देता है, उसमें बहुत बड़ा अन्तर है।
इसलिए साहित्य की परम्परा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिम्बित कराता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहां तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे सम्पत्तिशाली वर्गों की
देख-रेख में रचा है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिम्बित करता है, उसे भी परखकर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का। यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूप-रेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। जहाँ पूँजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया है, वहीं यह सम्भावना होती है कि सम्पत्तिशाली और सम्पत्ति हीन वर्ग एक-दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हों। पुराने साहित्य में वर्ग-हित साफ़-साफ़- टकराते हुए दिखाई दें, इसकी सम्भावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्त्वों की तरह साहित्य में ऐसे तत्त्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम में
आते हैं। आग की तरह जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्त्व बन गया है। कल-कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होती है और पूँजीवादी व्यवस्था में भी। सभ्यता का हर स्तर वर्गबद्ध नहीं होता। इसी तरह साहित्य का हर स्तर सम्पक्तिशाली वर्गों के हितों से बँधा हुआ नहीं रहता। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना क्योंकि इसका अविष्कार पूँजीवादी समाज में हुआ था। और उसका उपयोग भी पूँजीपतियों ने अपने हित में किया था।
साहित्य मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन से सम्बद्ध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत-सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणिमात्र से जोड़ती हैं। इस बात को बार-बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। उसमें मनुष्य का इन्द्रिय-बोध, उसकी भावनाएँ आन्तरिक प्रेरणाएँ भी व्यंजित होती हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है।
जिस समय ऐतिहासिक भौतिकता की स्थापना हुई, उस समय जीव-विज्ञान में विकासवाद का बोलबाला था। यह विकासवाद सही हो चाहे गलत, यह बात सच है कि साहित्य में विकास-प्रक्रिया उसी तरह सम्पन्न नहीं होती जैसे समाज में। सामाजिक विकास-क्रम में सामन्ती सभ्यता की अपेक्षा पूँजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है और पूँजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को। पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गयी है। पर यह आवश्यक नहीं है कि सामन्ती समाज के कवि की अपेक्षा पूँजीवादी समाज का
कवि श्रेष्ठ हो। यह भी सम्भव है कि आधुनिक सभ्यता विकास कविता का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा हो। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि-क्या भारत में और क्या यूरुप में –पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं और कहीं उनके आस-पास पहुँच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, वे उनका अनुकरण नहीं करते उससे सीखते हैं, और स्वयं नयी परम्पराओं को जन्म देते हैं। और जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए, वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृति असमर्थता का
सूचक होता है। जो महान साहित्यकार हैं, उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा को अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौन्दर्य ज्यों-का-त्यों नहीं रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अन्तर है। अमरीका ने ऐटमबम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज़ का उत्पादन दुबारा इग्लैंड में भी नहीं हुआ।
भौतिकवाद दो तरह का है, एक यान्त्रिक भौतिकवाद, दूसरा द्धन्द्धात्मक भौतिवाद। यान्त्रिक भौतिकवाद की की विशेषता यह है कि वह चेतना को आर्थिक सम्बन्धों का प्रतिबिम्ब मात्र मानता है। प्रतिबिम्ब यान्त्रिक होता ही है। जब चेतना प्रतिबिम्ब है, तब संस्कृति का ताना-बाना भी पूरी तरह बदल जाता है। इस यान्त्रिक भौतिकवाद का विकास फ्रान्स में हुआ; 19वीं सदी में जब भौतिक विज्ञान का विकास हुआ, तो इस विज्ञान का दार्शनिक दृष्टिकोण इसी यान्त्रिक
भौतिकवाद से प्रभावित हुआ। इसके विपरीत द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक सम्बन्धों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक सम्बन्धों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकता का अर्थ भाग्य-बाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं हो जाता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं हैं। दोनों का सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्षरूप में स्वाधीन होता है।
गुलामी अमरीका में थी और गुलामी एथेन्स में थी किन्तु एथेन्स की सभ्यता ने सारे यूरुप को प्रभावित किया और गुलामों के अमरीकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामन्तवाद दुनिया भर में कायम रहा। पर इस सामन्ती दुनिया में महान् कविता के दो ही केन्द्र थे- भारत और ईरान। पूँजीवादी विकास यूरुप के तमाम देशों में हुआ पर रैफेल, लेओनार्दों दा विंची और माइकेल ऐंजेलो इटली की देन हैं। यहां हम एक ओर यह देखते हैं कि विशेष सामाजिक
परिस्थितियों में कला का विकास सम्भव होता है, दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियाँ होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। जिस तरह औद्योगिक उत्पादन का समाजीकरण पूँजीवादी व्यवस्था में होता हैं, उस तरह साहित्यिक रचना का समाजिकरण नहीं होता। कारखाने में 1500 मज़दूर मिलकर दिन-प्रतिदिन थान के थान कपड़े निकाल सकते है। यदि साहित्यकारों को साहित्य-रचना के कारखाने में भर्ती कर दिया जाए तो हो सकता है कि उनके कुछ दोष दूर हो जायें, अथवा वे एक दूसरे से इतना लड़ें कि और किसी काम के लिए उन्हें फुरसत न मिले, पर नियमित रूप से उच्च कोटि के
उपन्यास, काव्य, नाटक के लिए उन्हें फुरसत न मिले, पर नियमित रूप से उच्च कोटि के उपन्यास, काव्य, नाटक, पंचवर्षीय योजना के अनुसार, उस कारखाने से निकलते रहेंगे, इसकी सम्भावना ज़रा कम है। साहित्यकार आपसी सहयोग से लाभ उठाते हैं पर अभी उस तकनीक का पता नहीं लगाया जा सका जिसे लोगों को सिखाकर साहित्य का सामूहिक उत्पादन किया जा सके।
साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। इसका यह अर्थ नहीं कि ये मनुष्य जो कुछ करते हैं। वह सब अच्छा ही अच्छा होता है, या उनके श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होते है। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। ऐसी कला निर्जीव होती है। इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफी निन्दा की जाती है। किन्तु जो लोग सबसे ज्यादा व्यक्ति-पूजा की निन्दा करते हैं, वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति-पूजा का प्रचार भी करते हैं। अन्तर इतना होता है कि ब्रह्मा की जगह उन्होंने विष्णु को बिठा दिया। लेकिन पूजा तो पूजा। ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यदि कोई भी
साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है, तो राजनीतिज्ञ यह दावा और भी नहीं कर सकते, इसलिए कि साहित्य के मूल्य, राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा, अधिक स्थायी हैं। अंग्रेज कवि टेनीसन ने लैटिन कवि वर्जिल कर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया। पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि-तरंगें हमें आज भी सुनायी देती हैं और हृदय को आनन्द-विह्यल कर देती हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानीदेवा v रह जायेगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शेली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नज़र आयेंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की उपेक्षा करोड़ों नयी आँखें देखेंगी।
साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह, जनसमुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि पुरुष के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है, वह अन्य किसी जाति की नहीं है। जनसमुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। प्राचीन यूनान अनेक गणसमाजों में बँटा हुआ था। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी
एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं ? 19वीं सदी में शेली और बायरन अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसी एकात्मकता पहचानने में बड़ा परिश्रम किया। भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि वह विच्छिन्न है और अविच्छिन्न भी। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्त्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परम्परा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
बंगाल विभाजित हुआ और है, किन्तु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परम्परा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए, तो ज्ञात हो जायेगा कि साहित्य की परम्परा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं।
एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएँ बोलनेवाले राष्ट्र की भी अस्मित होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं, अनेक भाषा-भाषी हैं। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्त्वों पर मुसीबत आती है, तब उन्हें अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान होता बहुत अच्छी तरह हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। सोवियत संघ के लोग हिटलर-विरोधी संग्राम को उचित ही महान् राष्ट्रीय (अथवा देशभक्तिपूर्ण) संग्राम कहते हैं। इस युद्ध के दौरान खासतौर से रूसी जाति ने
बार-बार अपनी साहित्य-परम्परा का स्मरण किया। सोवियत समाज ज़ारशाही रुस के समाज से भिन्न है। समाज-व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रवाह अविच्छन्न है। ज़ारशाही रूस जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान् साहित्यकार हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खण्डित नहीं होती वरन् और पुष्ट होती है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ है और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है जैसी वह 1917 से पहले नहीं थी। ज़ारशाही रूस में बहुत-सी जातियाँ पराधीन
बनाकर रखी गयी थीं। उन सब पर रूसी जाति के सामन्त और पूँजीपति शासन करते थे। जैसे और बहुत-से साम्राज्य होते हैं, वैसे ही यह भी साम्राज्य था। 1917 की क्रान्ति के बाद रूसी और गैररूसी जातियों के आपसी सम्बन्धों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत-सी जातियाँ सोवियत संघ में शामिल न हुईं, अलग हो गयीं। कुछ विलम्ब से, दूसरे महायुद्द से कुछ ही पहले, अन्य जातियाँ उसमें सामिल हुईं। सोवियत संघ में आज जितनी जातियाँ शामिल हैं, उनका वैसा मिला-जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है, जैसा भारत की जातियों का है। राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रवाह बहुत बड़ी
निर्धारक शक्ति है। यूरुप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं। पर यूरुप कभी राष्ट्र नहीं बना। और अब तो पूर्वी यूरुप और पश्चिमी यूरुप, दो यूरुप का अलग उल्लेख आम बात है। संसार का कोई भी देश, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से, इतिहास को ध्यान में रखें तो, भारत का मुकाबला नहीं कर सकता।
यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई। वह मुख्यतः संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति में रामायण और महाभारत को अलग कर दें, तो भारतीय साहित्य की आन्तरिक एकता टूट जायेगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही, जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकी की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परम्परा का मूल्यांकन उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i