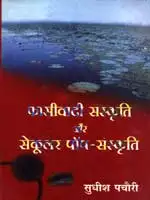|
संस्कृति >> फासीवादी संस्कृति और सेकुलर पॉप-संस्कृति फासीवादी संस्कृति और सेकुलर पॉप-संस्कृतिसुधीश पचौरी
|
37 पाठक हैं |
|||||||
यह ‘फासीवाद’ या ‘संस्कृति’ को लेकर एकेडेमिक या कोर्स-योग्य पुस्तक नहीं है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
यह ‘फासीवाद’ या ‘संस्कृति’ को लेकर
एकेडेमिक या
कोर्स-योग्य पुस्तक नहीं है। ऐसी किताबें ढेर सी हैं। लेकिन वे समकालीन
समाज में बनती, समाज को नियन्त्रित-उन्मादित-आन्दोलित करती
फासिस्टिक-सांस्कृतिक मुहिमों, उसके चिह्नों को पहचानने में कोई मदद नहीं
करतीं। उसके प्रभाव, उसके परास, उसके फैलाव को नहीं छूती।
उत्तर आधुनिक में ‘सांस्कृतिक राजनीति’ एक संघर्ष क्षेत्र बन उठा है। ‘सांस्कृतिक राजनीति’ करके ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’, मूलतः फासिस्ट संस्कृति और सत्ता बनाने को प्रयत्नशील है। उसकी मिसालें यत्र-यत्र-सर्वत्र दैनिक भाव से बनती है। वे इसके लिए ‘पॉपुलर कल्चर’ के चिह्नों का सहारा लेते हैं, माध्यमों का सहारा लेते हैं, जनता में पॉपुलर भावपक्ष का निर्माण कर उसे एक निरंकुश अन्धराष्ट्रवादी भाव में नियोजित करते रहते हैं।
इसके बरक्स, इसके प्रतिरोध में कार्यरत प्रगतिशील सेकूलर और मानवतावादी विचारों और सांस्कृतिक उपादानों, चिह्नों का लगातार क्षय नजर आता है। कुछ नए प्रतिरोधमूलक प्रयत्न नजर आते हैं तो वे अपने स्वरूप एवं प्रभाव क्षमता में ‘हाई कल्चर’ (एलीट) बनकर आते हैं, आम जनता का उनसे कोई आवश्यक संवाद-सम्बन्ध नहीं बनता।
सारा ‘पब्लिक स्पेस’ फासिस्टिक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी तत्त्वों के लिए खुला छूटा दिखता है जिसे वे दिन-रात भरते रहते हैं, यदि आम जनता में, विवेक की जगह अन्ध पूजा भाव, संवाद की जगह बदले और हिंसा का भाव रहता है तो इसलिए भी कि विकासहीनता से उपजी आत्महीनता और ग्लोबलाइजेशन के मुक्त कामना-संसार से उपजे अवसरवाद के बीच आदमी फँसा है। एक ओर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपनी अन्धताओं की लाठियों से इसे अपने नियन्त्रण में लेना चाहता है। दूसरी ओर ग्लोबलाइजेशन की प्रबल आर्थिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक शक्तियाँ उसे उसके अन्ध लोक अखिल भारतीय जेनरेशन नेक्स्ट सामने उभर आई है जो मीडिया प्रेरित, बाजार मित्र और ग्लोबल मिजाज की है। इस नए यथार्थ का जनक ‘लेट कैपीटलिज्म’ है और उसकी उत्तर आधुनिक ज्ञान-दशाएँ एवं ज्ञान-सरणियाँ हैं जो उसे किसी तरह के तत्त्ववाद, केन्द्रवाद और अतीत-जीविता से मुक्त कर उपभोक्ता क्षेत्र में ले आ रही है।
मनोरंजन उद्योग इस बदलाव का बड़ा माध्यम बन रहा है, फिल्में, टीवी सीरियल, अखबार, विज्ञापन, एफएम रेडियो, एल्बमें, गानों के रिमिक्स, रेगे, टैप भंगड़ा इत्यादि मनोरंजन के अनन्त रूप पॉप कल्चर के विराट वातावरण को बनाते हैं जिनमें शामिल युवा क्षेत्र अपनी अभिव्यक्ति करता है, और इस तरह पॉपूलर कल्चर के एक ही संलग्नकारी (इन्क्लूसिव) और ‘मुक्तकारी’ (एक्सक्लूसिव), बहुमुखी, बहुस्तरीय द्वन्द्वात्मकता में सक्रिय होता है। वह कथित भक्ति और अध्यात्म के इस देश में मैटीरियाल मैन बनता है और पॉपूलर कल्चर उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। इसी में वह अपना स्वत्व अपना हस्तक्षेप सम्भव पाता है। उसकी इस मुक्ति-कामना पर सबसे पहले तत्त्ववादी फासिस्ट हमले करते हैं। वे इसे अपनी सत्ता के लिए खतरा समझते हैं। वह है भी। लेकिन वे चालाकी से इन नए औजारों का सहारा भी लेते हैं। सेकूलर विमर्श इस पॉपुलर क्षेत्र में आने से भी डरता है।
इसीलिए राजनीतिक सेकूलर सत्ता सम्भव तो हो सकती है लेकिन पब्लिक स्फीयर तत्त्ववाद की अन्ध पूजा से भरा रहता है; इसे हम रोज़ाना के सत्ता समर्थित सांस्कृतिक इशारों में, विविध दलों के कार्यों में पा सकते हैं। सब मिलकर वे मुक्ति के नए जनतन्त्र को तुरन्त मर्यादित करने पर तुल जाते हैं।
सेक्स, आनन्द, सुख, उपभोग, ग्लोबल नागरिकता, स्वत्व-निजत्य की चिन्ता आदि वे नए भावबोध हैं जो दबे हुए, दमित सेक्सवाले समाज को खोलते हैं। ये ‘पॉपुलर कल्चर’ के नए तनाव बिन्दु हैं। वह उन्हें बराबर खोलती है। उन्हें ‘क्रिटिकल क्षेत्र’ में लाती है।
हमारे उपलब्ध साहित्यिक विमर्श अभी तक यथार्थवादी ‘पॉजीटिविज्म’ में फँसे हैं या रस छन्द अलंकार में फँसे हैं। वे राष्ट्रवादी संयम, नियन्त्रण को अन्धता तक ले जाते हैं जबकि वे जानते हैं कि इस ग्लोबल समय में वे एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं।
मार्क्स एंगेल्स ने 1948 में कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो में कहा था कि पूँजीपति वर्ग धरती के चप्पे-चप्पे को रौंद डालेगा, बदल डालेगा और बदलाव इतना तेज होगा कि जब तक हम एक बदलाव को पकड़ेंगे वह उसे भी बदल डालेंगे । बाद में ऑफिसियल मार्क्सवाद इस ‘ग्लोबलाइजेशन’ के मर्म को समझने की जगह मूलतः राष्ट्रवादी संस्करणों का पर्याय सा बन गया। पूँजीवाद ग्लोबल रहा। ग्लोबल मार्क्सवाद राष्ट्र-प्रेमी हो उठा। शायद वक्त का तकाजा रहा। राष्ट्रवाद के फँसते ही मार्क्सवादी विर्मश भी फँस गया। दरअसल वह ‘आधार’ और ‘अधिरचना’ वाली यान्त्रिक समझ और बहसों में ढेर हो गया। उसकी सांस्कृतिक समझ भी इसी यान्त्रिकता का शिकार हुई। समाजवादी यथार्थवादी के पेट से पतित पूँजीवादी यथार्थ निकल पड़ा।
तो भी ग्राम्शी, अल्थुसे से लेकर फ्रेंकफुर्त स्कूल और अब के उत्तर आधुनिक उत्तर संरचनावादी विर्मशकारों ने मार्क्सवादी सिद्धान्तिकी के उक्त यान्त्रिक अमल पर उँगली रखी तथा बहसों को चारों तरफ मुक्त किया। ‘कल्चरल थियरी’ इन्हीं विर्मशों में से एक है जो ‘पॉपुलर कल्चर’ को गम्भीरता से देखती है। इन टिप्पणियों में आपको उनकी छायाएँ मिलेंगी। वे ‘पॉपुलर कल्चर’ के रूपों एवं क्षेत्रों के समझने की कोशिश हैं। ‘पॉपुलर कल्चर’ चूँकि मूलतः और अन्ततः किसी भी तरह के तत्त्वाद के विपरीत कार्य करती है। इसीलिए वह हमेशा केन्द्रवाद तत्त्ववाद और फासीवाद के खिलाफ जगह बनाती है और उसके जनतन्त्र के विस्तार की माँग करती है। इस ‘क्रिटिकल’ जगह को तत्त्ववादियों के हड़पने के लिए यों ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस जगह में भी संघर्ष करना होगा क्योंकि यह अब निर्णायक क्षेत्र बन उठा है। ये टिप्पणियाँ इसी चिन्ता से प्रेरित हैं। इसमें मार्क्सवाद और उससे बाहर की बहसें हैं तो समकालीन जीवन में ‘पॉपुलर क्षणों’ के अनुभवों को देखने की कोशिश भी है। ‘पॉपुलर कल्चर’ निष्क्रिय गुलाम श्रोता-दर्शक नहीं बनाती, वह एक ऐसा जगत बनाती है जो ‘विमर्शात्मक’ होता है। उसे देखने के लिए पॉपुलर संस्कृति की समझ चाहिए।
यहाँ उपलब्ध टिप्पणियाँ इस दिशा में पाठकों की मदद कर सकती है : इनकी शैली अलग अलग है क्योंकि हर बार एक चंचल क्षण, एक चंचल जटिल यथार्थ को पकड़ने और विर्मश में लाने की कोशिश है।
उम्मीद है कि यह हिन्दी में ‘सांस्कृतिक अध्ययनों’ की दिशा में एक मामूली-सा क्षण बनाएगी। साहित्य अध्ययनों में अब सांस्कृतिक अध्ययन शामिल किए जाने का वक्त आ गया है। हिन्दी साहित्य के परम्परागत कलारूपों के साथ यदि हम हिन्दी की ‘पॉपुलर कल्चर’ के रूपों को भी पढ़ने-पढ़ाने का उद्यम करें तो हिन्दी क्षेत्र की मुक्ति के नए रास्ते खुलेंगे।
उत्तर आधुनिक में ‘सांस्कृतिक राजनीति’ एक संघर्ष क्षेत्र बन उठा है। ‘सांस्कृतिक राजनीति’ करके ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’, मूलतः फासिस्ट संस्कृति और सत्ता बनाने को प्रयत्नशील है। उसकी मिसालें यत्र-यत्र-सर्वत्र दैनिक भाव से बनती है। वे इसके लिए ‘पॉपुलर कल्चर’ के चिह्नों का सहारा लेते हैं, माध्यमों का सहारा लेते हैं, जनता में पॉपुलर भावपक्ष का निर्माण कर उसे एक निरंकुश अन्धराष्ट्रवादी भाव में नियोजित करते रहते हैं।
इसके बरक्स, इसके प्रतिरोध में कार्यरत प्रगतिशील सेकूलर और मानवतावादी विचारों और सांस्कृतिक उपादानों, चिह्नों का लगातार क्षय नजर आता है। कुछ नए प्रतिरोधमूलक प्रयत्न नजर आते हैं तो वे अपने स्वरूप एवं प्रभाव क्षमता में ‘हाई कल्चर’ (एलीट) बनकर आते हैं, आम जनता का उनसे कोई आवश्यक संवाद-सम्बन्ध नहीं बनता।
सारा ‘पब्लिक स्पेस’ फासिस्टिक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी तत्त्वों के लिए खुला छूटा दिखता है जिसे वे दिन-रात भरते रहते हैं, यदि आम जनता में, विवेक की जगह अन्ध पूजा भाव, संवाद की जगह बदले और हिंसा का भाव रहता है तो इसलिए भी कि विकासहीनता से उपजी आत्महीनता और ग्लोबलाइजेशन के मुक्त कामना-संसार से उपजे अवसरवाद के बीच आदमी फँसा है। एक ओर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपनी अन्धताओं की लाठियों से इसे अपने नियन्त्रण में लेना चाहता है। दूसरी ओर ग्लोबलाइजेशन की प्रबल आर्थिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक शक्तियाँ उसे उसके अन्ध लोक अखिल भारतीय जेनरेशन नेक्स्ट सामने उभर आई है जो मीडिया प्रेरित, बाजार मित्र और ग्लोबल मिजाज की है। इस नए यथार्थ का जनक ‘लेट कैपीटलिज्म’ है और उसकी उत्तर आधुनिक ज्ञान-दशाएँ एवं ज्ञान-सरणियाँ हैं जो उसे किसी तरह के तत्त्ववाद, केन्द्रवाद और अतीत-जीविता से मुक्त कर उपभोक्ता क्षेत्र में ले आ रही है।
मनोरंजन उद्योग इस बदलाव का बड़ा माध्यम बन रहा है, फिल्में, टीवी सीरियल, अखबार, विज्ञापन, एफएम रेडियो, एल्बमें, गानों के रिमिक्स, रेगे, टैप भंगड़ा इत्यादि मनोरंजन के अनन्त रूप पॉप कल्चर के विराट वातावरण को बनाते हैं जिनमें शामिल युवा क्षेत्र अपनी अभिव्यक्ति करता है, और इस तरह पॉपूलर कल्चर के एक ही संलग्नकारी (इन्क्लूसिव) और ‘मुक्तकारी’ (एक्सक्लूसिव), बहुमुखी, बहुस्तरीय द्वन्द्वात्मकता में सक्रिय होता है। वह कथित भक्ति और अध्यात्म के इस देश में मैटीरियाल मैन बनता है और पॉपूलर कल्चर उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। इसी में वह अपना स्वत्व अपना हस्तक्षेप सम्भव पाता है। उसकी इस मुक्ति-कामना पर सबसे पहले तत्त्ववादी फासिस्ट हमले करते हैं। वे इसे अपनी सत्ता के लिए खतरा समझते हैं। वह है भी। लेकिन वे चालाकी से इन नए औजारों का सहारा भी लेते हैं। सेकूलर विमर्श इस पॉपुलर क्षेत्र में आने से भी डरता है।
इसीलिए राजनीतिक सेकूलर सत्ता सम्भव तो हो सकती है लेकिन पब्लिक स्फीयर तत्त्ववाद की अन्ध पूजा से भरा रहता है; इसे हम रोज़ाना के सत्ता समर्थित सांस्कृतिक इशारों में, विविध दलों के कार्यों में पा सकते हैं। सब मिलकर वे मुक्ति के नए जनतन्त्र को तुरन्त मर्यादित करने पर तुल जाते हैं।
सेक्स, आनन्द, सुख, उपभोग, ग्लोबल नागरिकता, स्वत्व-निजत्य की चिन्ता आदि वे नए भावबोध हैं जो दबे हुए, दमित सेक्सवाले समाज को खोलते हैं। ये ‘पॉपुलर कल्चर’ के नए तनाव बिन्दु हैं। वह उन्हें बराबर खोलती है। उन्हें ‘क्रिटिकल क्षेत्र’ में लाती है।
हमारे उपलब्ध साहित्यिक विमर्श अभी तक यथार्थवादी ‘पॉजीटिविज्म’ में फँसे हैं या रस छन्द अलंकार में फँसे हैं। वे राष्ट्रवादी संयम, नियन्त्रण को अन्धता तक ले जाते हैं जबकि वे जानते हैं कि इस ग्लोबल समय में वे एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं।
मार्क्स एंगेल्स ने 1948 में कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो में कहा था कि पूँजीपति वर्ग धरती के चप्पे-चप्पे को रौंद डालेगा, बदल डालेगा और बदलाव इतना तेज होगा कि जब तक हम एक बदलाव को पकड़ेंगे वह उसे भी बदल डालेंगे । बाद में ऑफिसियल मार्क्सवाद इस ‘ग्लोबलाइजेशन’ के मर्म को समझने की जगह मूलतः राष्ट्रवादी संस्करणों का पर्याय सा बन गया। पूँजीवाद ग्लोबल रहा। ग्लोबल मार्क्सवाद राष्ट्र-प्रेमी हो उठा। शायद वक्त का तकाजा रहा। राष्ट्रवाद के फँसते ही मार्क्सवादी विर्मश भी फँस गया। दरअसल वह ‘आधार’ और ‘अधिरचना’ वाली यान्त्रिक समझ और बहसों में ढेर हो गया। उसकी सांस्कृतिक समझ भी इसी यान्त्रिकता का शिकार हुई। समाजवादी यथार्थवादी के पेट से पतित पूँजीवादी यथार्थ निकल पड़ा।
तो भी ग्राम्शी, अल्थुसे से लेकर फ्रेंकफुर्त स्कूल और अब के उत्तर आधुनिक उत्तर संरचनावादी विर्मशकारों ने मार्क्सवादी सिद्धान्तिकी के उक्त यान्त्रिक अमल पर उँगली रखी तथा बहसों को चारों तरफ मुक्त किया। ‘कल्चरल थियरी’ इन्हीं विर्मशों में से एक है जो ‘पॉपुलर कल्चर’ को गम्भीरता से देखती है। इन टिप्पणियों में आपको उनकी छायाएँ मिलेंगी। वे ‘पॉपुलर कल्चर’ के रूपों एवं क्षेत्रों के समझने की कोशिश हैं। ‘पॉपुलर कल्चर’ चूँकि मूलतः और अन्ततः किसी भी तरह के तत्त्वाद के विपरीत कार्य करती है। इसीलिए वह हमेशा केन्द्रवाद तत्त्ववाद और फासीवाद के खिलाफ जगह बनाती है और उसके जनतन्त्र के विस्तार की माँग करती है। इस ‘क्रिटिकल’ जगह को तत्त्ववादियों के हड़पने के लिए यों ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस जगह में भी संघर्ष करना होगा क्योंकि यह अब निर्णायक क्षेत्र बन उठा है। ये टिप्पणियाँ इसी चिन्ता से प्रेरित हैं। इसमें मार्क्सवाद और उससे बाहर की बहसें हैं तो समकालीन जीवन में ‘पॉपुलर क्षणों’ के अनुभवों को देखने की कोशिश भी है। ‘पॉपुलर कल्चर’ निष्क्रिय गुलाम श्रोता-दर्शक नहीं बनाती, वह एक ऐसा जगत बनाती है जो ‘विमर्शात्मक’ होता है। उसे देखने के लिए पॉपुलर संस्कृति की समझ चाहिए।
यहाँ उपलब्ध टिप्पणियाँ इस दिशा में पाठकों की मदद कर सकती है : इनकी शैली अलग अलग है क्योंकि हर बार एक चंचल क्षण, एक चंचल जटिल यथार्थ को पकड़ने और विर्मश में लाने की कोशिश है।
उम्मीद है कि यह हिन्दी में ‘सांस्कृतिक अध्ययनों’ की दिशा में एक मामूली-सा क्षण बनाएगी। साहित्य अध्ययनों में अब सांस्कृतिक अध्ययन शामिल किए जाने का वक्त आ गया है। हिन्दी साहित्य के परम्परागत कलारूपों के साथ यदि हम हिन्दी की ‘पॉपुलर कल्चर’ के रूपों को भी पढ़ने-पढ़ाने का उद्यम करें तो हिन्दी क्षेत्र की मुक्ति के नए रास्ते खुलेंगे।
सुधीश पचौरी
उत्तर आधुनिक भाव बोध और पॉपुलर कल्चर
एक नजर से देखें तो उत्तर-आधुनिकतावाद और पॉप कल्चर एक दूसरे से मिले-जुले
बढ़े हैं। अमेरिकी संस्कृति समीक्षक सुजन सौंटाग ने 1996 में अपनी कृति
‘अगेन्स्ट इंटरप्रेटेशंस’ में सम्भवतः सबसे पहले लिखा
कि हम
एक नए भावबोध उत्तर आधुनिक भावबोध में आ गए हैं : नए भावबोध का सबसे
महत्त्वपूर्ण परिणाम एक प्रकार का नया भावबोध है जिसमें
‘उच्च’ संस्कृतिक और निम्न संस्कृति का भेद निरर्थक
होता जाता
है।’
जॉन स्टोरी का लेख : पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पॉपुलर कल्चर (पेज-147, पुस्तक ‘रूटलेज कंपेनियन टू पोस्ट मॉडर्निज्म’ से उद्धृत सम्पादक स्टुआर्ट सिम।)
इस कॉलम के पाठक जानते हैं कि इस लेखक ने पॉपुलर कल्चर में ‘उच्च’ और ‘निम्न’ के लिए अभेद के बारे में लगातार बताया है। ‘जनसमाज’ बनेंगे तो ‘जनसंस्कृति’ बनेगी और इस तरह आधुनिकतावादी चरण के ‘उच्च’ कलामानक व्यर्थ होकर निम्न यानी सामान्य मानकों जो अन्ततः और प्रथमतः ‘माँग और पूर्ति’ के नियम से संचालित होते हैं-में मिक्स हो जाएँगे। मसलन एम.एफ. हुसैन फिल्म बनाने लगेंगे, न्यूज में रहने को आतुर होंगे, पॉपुलर माधुरी के सहारे कला करेंगे। इन दिनों मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास व बंगलौर ही नहीं दूसरे दर्जे के महानगरों में भी हमें उच्च कलावन्तों और उनके निम्न कला अनुरोधों कि हमें आडिएंस चाहिए, रिकार्ड एलबम बनने चाहिए, हम बिकने चाहिए का मिक्स दिखता है। एक शुभा मुदग्ल ही एलबम नहीं बनाती हैं। सब इसी ‘मिक्स’ में रहना चाहते हैं। इन दिनों कलाकार (उच्च कलाकार) सबसे पहले निम्न बाजार पर नजर रखता है। यह दृश्य बहुत उपलब्ध बीहड़ और स्वयं पॉपुलर हैं।
अजीब बात लगेगी अगर हम कहें कि उत्तर भारत में, खासकर हिन्दी संस्कृति में उच्च और निम्न का वैसा सुदृढ़ भेद कभी नहीं दिखा जैसा कि यूरोप आदि में कल तक दिखता था। यों कलात्मकता और लोकप्रियता हमेशा ही भिन्न स्थिति के पद बने रहे। लेकिन भारत का नाट्यशास्त्र तो इसी अन्योन्यता का पहला ग्रन्थ रहा। इस क्रम को हम देख सकते हैं और साहित्य-संस्कृति के इतिहास से पर्याप्त पोषक उदाहरण दिए जा सकते हैं। तब भी यदि कुछ कहते हैं कि आप संस्कृति पर उत्तर-आधुनिक पदावली लागू करके ‘पश्चिम पश्चिम’ कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाए ? सांस्कृतिक बोध की पदावलियाँ स्थानीय होते हुए भी ग्लोबल होती हैं और ऐसा कुछ भी ग्लोबल नहीं होता जो स्थानीयता लिए न आए। ऐसे में यदि उत्तर आधुनिकता अपने पॉपुलर कल्चर और उसकी प्रक्रिया को समझने में मदद करती है, उसकी भूमिका को स्पष्ट करती है, उसके उपयोगिता-मूल्य को स्पष्ट करती है तो हमें उसे समझना चाहिए। इस क्रम में उत्तर आधुनिक विमर्शों में ‘पॉपुलर कल्चर’ के विचार को देखना अप्रासंगिक नहीं होगा।
याद करें, उत्तर आधुनिक चिन्तक फ्रांसुआ ल्योतार ने जब ‘महावृत्तान्तों’ के बारे में अपने ‘सन्देह’ जताते हैं और उत्तर आधुनिक ज्ञानावस्थाओं की चर्चा करते हैं तो वे नई ज्ञानावस्था व भावबोध मे ‘महानता’ के होने पर ‘सन्देह’ करते हैं। यह बुद्धिजीवी, के प्रतिरोधात्मक नकारात्मक हीरोइज्म पर ही सन्देह करना है। (इन दिनों हिन्दी के बुद्धिजीवियों कलावन्तों की कुल स्थिति विश्वसनीय न होकर सन्दिग्ध ही है जो स्वयं एक उत्तर आधुनिक स्थिति है, भले बुद्धिजीवी स्वयं को उत्तर आधुनिक न मानें, लेकिन उनकी भूमिका का पतन उन्हें उत्तर आधुनिक ‘परनाले’ में फेंक ही देती है।) यूरोप और अमेरिका आदि समाजों में बुद्धिजीवी के ‘नायकत्व’ के ऐसे ही तन पर टिप्पणी करते हुए इयान चैम्बर्स ने ‘पॉपुलर कल्चर’ (1988) में लिखा कि उत्तर-आधुनिक पर होनेवाली बहस, अंशतः ‘पॉपुलर कल्चर’ की ‘उपद्रवी घुसपैठ’ का लक्षण है। यह ‘घुसपैठ’ दरअसल पूर्वकालीन विशेषाधिकृत उच्च कलाक्षेत्रों में हुई है। ज्ञान और सांस्कृतिक वितरण के नए पॉपुलर नेटवर्क के सामने कल तक की सिद्धान्तिकियाँ लड़खड़ा रही हैं, स्थिति की व्याख्या करने, समझाने की बुद्धिजीवी की भूमिका तक खतरे में है।’ (उद्धृत वही 148-149)
हिन्दी में बाजार, भूमंडलीकरण, उत्तर-आधुनिकता को लेकर यत्र-तत्र प्रकट प्रतिक्रियाएँ इसी ‘खतरे’ को बताती हैं। तेज बदलते जगत को हमारे उपलब्ध बुद्धिजीवी समझ-समझा नहीं पा रहे। ढेर सारी प्रतिक्रियाएँ ‘खिसियाने’ की मुद्रा पर नजर आती हैं। ऐसा ही पश्चिम में यन्त्र-तन्त्र दिखने में आता है। और यहीं एक अजीब बात पैदा होती है।
पॉपुलर कल्चर में, जैसा कि एंजेला मैकरोबी ने ‘पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पॉपुलर’ कल्चर में कहा है कि पॉपुलर कल्चर, उत्तर आधुनिक स्थितियों में उन आवाजों का कलराव है, जिन्हें आधुनिकतावादी महावृत्तान्तों ने दबा दफना दिया था, जो मूलतः साम्राज्यवादी और पितृसत्तात्मक थे। (वही, पेज 149)
आधुनिकतावादी अपनी मुक्ति के लिए एक जनता की बात करते रहे लेकिन जनता की जरूरत के लिए कलासंस्कृति और उनके माध्यम जब सर्वसुलभ होने की स्थिति में आए तब वही इसे ‘पतन’ कहने लगे। जनता को सांस्कृतिक प्रारूप अधिक उपलब्ध हों यही तो संकल्प था। और जब यह तकनीक बाजार और माध्यमों से सम्भव हो रहा है तो यह परेशानी का विषय है। इस तरह संस्कृति में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दबावों का द्वन्द्व अनेक बुद्धिजीवियों को बेकार कर रहा है। स्टुआर्ट सिम सच कहते हैं कि वर्चस्वकारी महावृत्तान्तों में दबे स्थानीयतावादी, लिंगवादी, धार्मिक वर्गीय, यौनिक विमर्श हाशियों की जगहों से उठ रहे हैं। एक दूसरे को काटते हुए ये विमर्श कुछ भी साबुत नहीं छोड़ते। यह उपद्रव उत्तर-आधुनिक है जो पॉपुलर कल्चर के क्षेत्र में सर्वाधिक दृष्टव्य है। इसे देखकर को बेना मर्कर ने ‘वैलकम टू जंगल’ नामक अपने ग्रन्थ (1994) में कहा कि अफ्रीकी कैरीबियाई और एशियाई जनों की नई आवाजें, व्यवहार और अस्मिताएँ जो उत्तर साम्राज्यी ब्रिटेन के हाशियों से उभरकर आ रही है और ‘निश्चल’, ‘सहमतिमूलक सत्यों’ को उपद्रवग्रस्त कर रही हैं और इस तरह बोध के नए मार्गों को खोल रही हैं। (वही, 149) इस नई ‘भिन्नता’ और ‘विविधता’ के उभार को ब्रिटेन के सन्दर्भ में भिखु पारिख ने ‘मल्टी कल्चरिज्म’ के रूप में देखा और नए किस्म के जनतन्त्र को रेखांकित किया।
‘रिथिंकिंग मल्टी कल्चरिज्म’ (2000) में भिखु पारिख प्रकारान्तर से इस नए सांस्कृतिक संवाद या विमर्श की ही बात करते हैं। भारत के सन्दर्भ में; चाहे हिन्दू केन्द्रिक विमर्श-विविध विशिष्ट अल्प सांस्कृतिक आवाजों को ‘हिन्दुत्व’ के ‘सम्प्रदाय’ कहे या सेकूलर विपक्ष ‘अनेकता में एकता’ की बात करे, उभर रही, बहुत सारी ‘आवाजों’ के ‘होने’ को जरूर मानते हैं। लेकिन उनके होने को, या उनके ज्यादा मुखर होने को अपने केन्द्रवाद के लिए खतरा मानते हैं। उत्तर-आधुनिकता में केन्द्रवाद के बरक्स विकेन्द्रण पर जोर दरअसल इन्हीं लोकप्रिय केन्द्रापसारित विमर्शों का दूसरा नाम है। और चूँकि केन्द्रवादी विमर्श अभी भी अपने केन्द्रवाद से चिपके रहना चाहते हैं इसलिए वे नए हाशिए वाले विमर्शों को हतोत्साहित किया करते हैं। आश्चर्य कि वे विभिन्नता को मानते हैं लेकिन ‘विभिन्नता’ को उसके आत्मरूप में प्रकट नहीं होने देना चाहते।
यदि हम ज्यां बौद्रीआ के ‘साइमलक्रा एंड साइमूलेशंस’ (1981) ग्रन्थ को याद करें तो हमें उत्तर आधुनिक पदावली में ‘हाइपर रीयल’ पद मिलता है जो ‘पॉपुलर कल्चर’ के विमर्शों से उनके यहाँ पहुँचा है। स्वयं ‘साइमूलेशंस’ पद ‘प्रपंच’, ‘छाया’, ‘नकल’, ‘प्रतिबिम्ब’, ‘छलना’ का अर्थ देता है जो आज की उपभोक्ता संस्कृति से जुड़े उपादन बनाते हैं। बौद्रीआ इस प्रपंच को अति आघाती अति दुहराववाली यानी ‘हाइपर’ प्रक्रिया मानते हैं। हाइपर रीयल यानी ऐसा यथार्थ या सच जो अस्थिर, चंचल, तरल और आवेगमय हो। इसे हम टीवी के प्रपंच से समझ सकते हैं और तमाम सांस्कृतिक उपक्रमों के टीवीमय हो जाने के सन्दर्भ में पढ़ सकते हैं।
बौद्रीआ के यहाँ ‘उपभोक्ता संस्कृति’ में पॉपुलर कल्चर के चिह्न अपना उत्तर आधुनिक संस्कार पा लेते हैं। उच्च और निम्न का भेद यहाँ किस तरह मिटता है और किस तरह की निरन्तर अतृप्ति उपभोग के बावजूद रहती है और किस तरह यह तृप्ति और अतृप्ति की निरन्तरता एक विराट हाइपर-रीयल को बनाती रहती है इस पर बौद्रीआ ने इस दौर के तमाम अन्य चिन्तकों से ज्यादा काम किया है। वे उस पुस्तक में कहते हैं कि उपभोक्ता संस्कृति में ‘वस्तु’ और उसके ‘प्रतिनिधान’ के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। अन्तर्वस्तु और रूप शैली का फर्क मिट जाता है। यथार्थ की जगह उसकी अनन्त प्रतिच्छवियाँ ले लेती हैं, वे अपने से बाहर किसी सन्दर्भ को रहने नहीं देती। वे अपने में एक यथार्थ होती हैं। यह ‘साइमूलेशन’ ‘उपन्यास’ या ‘कहानी’ के ‘सच’ या ‘झूठ’ से अलग होता है। यह ‘झूठ’ को ‘सच’ ही नहीं बनाता, यह यथार्थ से अपनी समानता सम्बन्ध या तुलना सम्बन्धों को भी मना करता है। यह जगत ‘आत्म सन्दर्भित’ जगत होता है। यह ‘प्रपंच’ का जगत होता है। (ज्यां बौद्रीआ, सलेक्टेड राइटिंग सम्पादक मार्क पॉस्टप पेज 5-6)
यह ‘प्रपंच’, यह साइमूलेशंस, अपने सन्दर्भ की प्रपंची निरन्तरता में प्रायः यथार्थ से भी ज्यादा सच नजर आते हैं। ये पॉपुलर कल्चर में लगातार बनते हैं, जो ‘यथार्थ’ से ‘बेहतर’ नजर आती हैं। यही ‘हाइपर रीयलिज्म’ की विशेषता है जो इन दिनों हर तरफ व्याप्त नजर आती है। लोग टीवी देखकर, सोप ओपेरा देखकर, उनमें बनाए गए चरित्रों के ‘फैन’ बनकर पत्र लिखते हैं, उनसे हमदर्दी रखते हैं जबकि वे यथार्थ में नहीं होते। वे उनसे मिलना चाहते हैं अपने यहाँ। इन दिनों शादियों में लोग डोनाल्ड डक को बुलाते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं। ऐसे अनेक चरित्र जीवन में और जीवन उनमें घुस जाता है जबकि वे ‘यथार्थ’ नहीं होते। बौद्रीआ इस स्थिति को जीवन में टीवी का खपना और टीवी में जीवन का खपना कहते हैं। इसे हम भक्तों में उनके ‘उन्माद’ से देखते हैं, ‘उन्माद’ में भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता दूरी समाप्त कर देता है। पॉपुलर कल्चर उसके माध्यम के यथार्थ और प्रतिनिधान यानी प्रतिबिम्बन के बीच ऐसा ही ‘अ-भेद’ पैदा करती है। पॉपुलर कल्चर इस अभेद को स्थापित करती है।
इस क्रम में ‘पॉपुलर कल्चर’ के प्रगतिशील विद्वान जॉन फिस्के ने अपनी पुस्तक ‘मीडिया मैटर्स’ (1994) में कहा है कि पोस्ट मॉर्डन मीडिया यथार्थ के दोयम प्रतिनिधान नहीं देता। वे उस यथार्थ को बनाते हैं जिसका वे प्रतिनिधान करते हैं। जो भी ‘घटनाएँ’, होती हैं वे ‘मीडिया घटित’ होती हैं। अमेरिका में खिलाड़ी ओ.जे. सिंपसन की गिरफ्तारी इस ‘पॉपुलर कल्चर’ और ‘हाइपर रीयल’ की अन्यतम उदाहरण है। जॉन फिस्के बताते हैं कि किस तरह ‘स्थानीय लोग जो अपने घरों में टीवी पर किसी ‘चेन’ को देख रहे थे वे सब ओ.जे. सिंपसन के घर की ओर चल पड़े। वे अपने साथ अपने पोर्टेबल टीवी सैट ले गए। वे सारी घटना को (सिंपसन की गिरफ्तारी और मुकदमे को, उसके द्वारा किए गए कत्ल की पुनर्रचना को), ‘जीवित’ (लाइव) देखना चाहते थे लेकिन जानते थे कि टीवी पर उसका प्रसारण उस घटना का पूरक है। अपने आपको टीवी पर घटना को देखता देखकर, वे अपने आपको ही हाथ हिलाते थे। पोस्टमॉर्डन मनुष्य को एक साथ इस ही क्षण ‘लाइव पीपल’ और ‘मीडिया पीपल’ बनने में कोई दिक्कत नहीं होती। वे जानते थे कि मीडिया खबर ‘देता’ नहीं है, उसका निर्माण करता है, इसलिए सिंपसन की गिरफ्तारी खबर का हिस्सा बनने के लिए, सिर्फ ‘ऑन द स्पॉट’ होना ही काफी नहीं था उसे टीवी में भी दिखना जरूरी था। पूरा मुकदमा भी इसी तरह ‘दिखा’ ‘बना’ मुकदमा था। वह कोर्ट के लिए उतना नहीं बनाया गया जितना टीवी के लिए बनाया गया था।
अपने टीवी चैनलों पर कैमरे के फ्रेम के भीतर झाँकनेवाले लोगों को याद करें। वे क्यों टीवी में दिखना-होना चाहते हैं ? पॉपुलर होने के लिए कि लोग उन्हें जानें, देखें। इससे उनका ‘पावर’ बढ़ता है। अनेक घटनाएँ कुछ इस तरह की जाने लगी हैं कि वे पॉपुलर होने के लिए उचित उपयुक्त छवि दे सकें, रूप दे सकें। हमारे समाज में इन दिनों ऐसी अनन्त घटनाएँ होती हैं जो जितनी जीवन के लिए होती हैं, उतनी या कभी-कभी उससे ज्यादा टीवी की खातिर की जाती हैं। कोई मीनार पर चढ़ जाता है, कोई डिजाइनर सूट में रहता है, कोई टीवी के लिए सजग होकर बोलता है। सब पॉपुलर होने दिखने के लिए।
इस तरह, ‘पॉपुलर कल्चर’, इस बिन्दु पर आकर ‘आत्मोभोग’ बन जाती है। आप अपने से बाहर ‘पॉपुलर’ नहीं पाते, अपने में ही उसे पाते हैं। छलना में, प्रपंच में जाना, जाने की बढ़ती ललक, स्वयं को सहज यथार्थ से काटकर बनाए यथार्थ में ले आना, बनाए अति चंचल यथार्थ में हिस्सेदार बना लेना नितान्त नया सांस्कृतिक अनुभव एवं बोध है। इसे पोस्ट मॉर्डन भावबोध कहा जा सकता है। यह तो एक उदाहरण है जो यहाँ इसलिए दिया गया है कि टीवी सन्दर्भ सुर्वसुलभ है। उत्तर आधुनिक भावबोध के, पॉपुलर कल्चर में ‘खप’ जाने के अनेक प्रसंग बताए जा सकते हैं।
जॉन स्टोरी का लेख : पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पॉपुलर कल्चर (पेज-147, पुस्तक ‘रूटलेज कंपेनियन टू पोस्ट मॉडर्निज्म’ से उद्धृत सम्पादक स्टुआर्ट सिम।)
इस कॉलम के पाठक जानते हैं कि इस लेखक ने पॉपुलर कल्चर में ‘उच्च’ और ‘निम्न’ के लिए अभेद के बारे में लगातार बताया है। ‘जनसमाज’ बनेंगे तो ‘जनसंस्कृति’ बनेगी और इस तरह आधुनिकतावादी चरण के ‘उच्च’ कलामानक व्यर्थ होकर निम्न यानी सामान्य मानकों जो अन्ततः और प्रथमतः ‘माँग और पूर्ति’ के नियम से संचालित होते हैं-में मिक्स हो जाएँगे। मसलन एम.एफ. हुसैन फिल्म बनाने लगेंगे, न्यूज में रहने को आतुर होंगे, पॉपुलर माधुरी के सहारे कला करेंगे। इन दिनों मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास व बंगलौर ही नहीं दूसरे दर्जे के महानगरों में भी हमें उच्च कलावन्तों और उनके निम्न कला अनुरोधों कि हमें आडिएंस चाहिए, रिकार्ड एलबम बनने चाहिए, हम बिकने चाहिए का मिक्स दिखता है। एक शुभा मुदग्ल ही एलबम नहीं बनाती हैं। सब इसी ‘मिक्स’ में रहना चाहते हैं। इन दिनों कलाकार (उच्च कलाकार) सबसे पहले निम्न बाजार पर नजर रखता है। यह दृश्य बहुत उपलब्ध बीहड़ और स्वयं पॉपुलर हैं।
अजीब बात लगेगी अगर हम कहें कि उत्तर भारत में, खासकर हिन्दी संस्कृति में उच्च और निम्न का वैसा सुदृढ़ भेद कभी नहीं दिखा जैसा कि यूरोप आदि में कल तक दिखता था। यों कलात्मकता और लोकप्रियता हमेशा ही भिन्न स्थिति के पद बने रहे। लेकिन भारत का नाट्यशास्त्र तो इसी अन्योन्यता का पहला ग्रन्थ रहा। इस क्रम को हम देख सकते हैं और साहित्य-संस्कृति के इतिहास से पर्याप्त पोषक उदाहरण दिए जा सकते हैं। तब भी यदि कुछ कहते हैं कि आप संस्कृति पर उत्तर-आधुनिक पदावली लागू करके ‘पश्चिम पश्चिम’ कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाए ? सांस्कृतिक बोध की पदावलियाँ स्थानीय होते हुए भी ग्लोबल होती हैं और ऐसा कुछ भी ग्लोबल नहीं होता जो स्थानीयता लिए न आए। ऐसे में यदि उत्तर आधुनिकता अपने पॉपुलर कल्चर और उसकी प्रक्रिया को समझने में मदद करती है, उसकी भूमिका को स्पष्ट करती है, उसके उपयोगिता-मूल्य को स्पष्ट करती है तो हमें उसे समझना चाहिए। इस क्रम में उत्तर आधुनिक विमर्शों में ‘पॉपुलर कल्चर’ के विचार को देखना अप्रासंगिक नहीं होगा।
याद करें, उत्तर आधुनिक चिन्तक फ्रांसुआ ल्योतार ने जब ‘महावृत्तान्तों’ के बारे में अपने ‘सन्देह’ जताते हैं और उत्तर आधुनिक ज्ञानावस्थाओं की चर्चा करते हैं तो वे नई ज्ञानावस्था व भावबोध मे ‘महानता’ के होने पर ‘सन्देह’ करते हैं। यह बुद्धिजीवी, के प्रतिरोधात्मक नकारात्मक हीरोइज्म पर ही सन्देह करना है। (इन दिनों हिन्दी के बुद्धिजीवियों कलावन्तों की कुल स्थिति विश्वसनीय न होकर सन्दिग्ध ही है जो स्वयं एक उत्तर आधुनिक स्थिति है, भले बुद्धिजीवी स्वयं को उत्तर आधुनिक न मानें, लेकिन उनकी भूमिका का पतन उन्हें उत्तर आधुनिक ‘परनाले’ में फेंक ही देती है।) यूरोप और अमेरिका आदि समाजों में बुद्धिजीवी के ‘नायकत्व’ के ऐसे ही तन पर टिप्पणी करते हुए इयान चैम्बर्स ने ‘पॉपुलर कल्चर’ (1988) में लिखा कि उत्तर-आधुनिक पर होनेवाली बहस, अंशतः ‘पॉपुलर कल्चर’ की ‘उपद्रवी घुसपैठ’ का लक्षण है। यह ‘घुसपैठ’ दरअसल पूर्वकालीन विशेषाधिकृत उच्च कलाक्षेत्रों में हुई है। ज्ञान और सांस्कृतिक वितरण के नए पॉपुलर नेटवर्क के सामने कल तक की सिद्धान्तिकियाँ लड़खड़ा रही हैं, स्थिति की व्याख्या करने, समझाने की बुद्धिजीवी की भूमिका तक खतरे में है।’ (उद्धृत वही 148-149)
हिन्दी में बाजार, भूमंडलीकरण, उत्तर-आधुनिकता को लेकर यत्र-तत्र प्रकट प्रतिक्रियाएँ इसी ‘खतरे’ को बताती हैं। तेज बदलते जगत को हमारे उपलब्ध बुद्धिजीवी समझ-समझा नहीं पा रहे। ढेर सारी प्रतिक्रियाएँ ‘खिसियाने’ की मुद्रा पर नजर आती हैं। ऐसा ही पश्चिम में यन्त्र-तन्त्र दिखने में आता है। और यहीं एक अजीब बात पैदा होती है।
पॉपुलर कल्चर में, जैसा कि एंजेला मैकरोबी ने ‘पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पॉपुलर’ कल्चर में कहा है कि पॉपुलर कल्चर, उत्तर आधुनिक स्थितियों में उन आवाजों का कलराव है, जिन्हें आधुनिकतावादी महावृत्तान्तों ने दबा दफना दिया था, जो मूलतः साम्राज्यवादी और पितृसत्तात्मक थे। (वही, पेज 149)
आधुनिकतावादी अपनी मुक्ति के लिए एक जनता की बात करते रहे लेकिन जनता की जरूरत के लिए कलासंस्कृति और उनके माध्यम जब सर्वसुलभ होने की स्थिति में आए तब वही इसे ‘पतन’ कहने लगे। जनता को सांस्कृतिक प्रारूप अधिक उपलब्ध हों यही तो संकल्प था। और जब यह तकनीक बाजार और माध्यमों से सम्भव हो रहा है तो यह परेशानी का विषय है। इस तरह संस्कृति में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दबावों का द्वन्द्व अनेक बुद्धिजीवियों को बेकार कर रहा है। स्टुआर्ट सिम सच कहते हैं कि वर्चस्वकारी महावृत्तान्तों में दबे स्थानीयतावादी, लिंगवादी, धार्मिक वर्गीय, यौनिक विमर्श हाशियों की जगहों से उठ रहे हैं। एक दूसरे को काटते हुए ये विमर्श कुछ भी साबुत नहीं छोड़ते। यह उपद्रव उत्तर-आधुनिक है जो पॉपुलर कल्चर के क्षेत्र में सर्वाधिक दृष्टव्य है। इसे देखकर को बेना मर्कर ने ‘वैलकम टू जंगल’ नामक अपने ग्रन्थ (1994) में कहा कि अफ्रीकी कैरीबियाई और एशियाई जनों की नई आवाजें, व्यवहार और अस्मिताएँ जो उत्तर साम्राज्यी ब्रिटेन के हाशियों से उभरकर आ रही है और ‘निश्चल’, ‘सहमतिमूलक सत्यों’ को उपद्रवग्रस्त कर रही हैं और इस तरह बोध के नए मार्गों को खोल रही हैं। (वही, 149) इस नई ‘भिन्नता’ और ‘विविधता’ के उभार को ब्रिटेन के सन्दर्भ में भिखु पारिख ने ‘मल्टी कल्चरिज्म’ के रूप में देखा और नए किस्म के जनतन्त्र को रेखांकित किया।
‘रिथिंकिंग मल्टी कल्चरिज्म’ (2000) में भिखु पारिख प्रकारान्तर से इस नए सांस्कृतिक संवाद या विमर्श की ही बात करते हैं। भारत के सन्दर्भ में; चाहे हिन्दू केन्द्रिक विमर्श-विविध विशिष्ट अल्प सांस्कृतिक आवाजों को ‘हिन्दुत्व’ के ‘सम्प्रदाय’ कहे या सेकूलर विपक्ष ‘अनेकता में एकता’ की बात करे, उभर रही, बहुत सारी ‘आवाजों’ के ‘होने’ को जरूर मानते हैं। लेकिन उनके होने को, या उनके ज्यादा मुखर होने को अपने केन्द्रवाद के लिए खतरा मानते हैं। उत्तर-आधुनिकता में केन्द्रवाद के बरक्स विकेन्द्रण पर जोर दरअसल इन्हीं लोकप्रिय केन्द्रापसारित विमर्शों का दूसरा नाम है। और चूँकि केन्द्रवादी विमर्श अभी भी अपने केन्द्रवाद से चिपके रहना चाहते हैं इसलिए वे नए हाशिए वाले विमर्शों को हतोत्साहित किया करते हैं। आश्चर्य कि वे विभिन्नता को मानते हैं लेकिन ‘विभिन्नता’ को उसके आत्मरूप में प्रकट नहीं होने देना चाहते।
यदि हम ज्यां बौद्रीआ के ‘साइमलक्रा एंड साइमूलेशंस’ (1981) ग्रन्थ को याद करें तो हमें उत्तर आधुनिक पदावली में ‘हाइपर रीयल’ पद मिलता है जो ‘पॉपुलर कल्चर’ के विमर्शों से उनके यहाँ पहुँचा है। स्वयं ‘साइमूलेशंस’ पद ‘प्रपंच’, ‘छाया’, ‘नकल’, ‘प्रतिबिम्ब’, ‘छलना’ का अर्थ देता है जो आज की उपभोक्ता संस्कृति से जुड़े उपादन बनाते हैं। बौद्रीआ इस प्रपंच को अति आघाती अति दुहराववाली यानी ‘हाइपर’ प्रक्रिया मानते हैं। हाइपर रीयल यानी ऐसा यथार्थ या सच जो अस्थिर, चंचल, तरल और आवेगमय हो। इसे हम टीवी के प्रपंच से समझ सकते हैं और तमाम सांस्कृतिक उपक्रमों के टीवीमय हो जाने के सन्दर्भ में पढ़ सकते हैं।
बौद्रीआ के यहाँ ‘उपभोक्ता संस्कृति’ में पॉपुलर कल्चर के चिह्न अपना उत्तर आधुनिक संस्कार पा लेते हैं। उच्च और निम्न का भेद यहाँ किस तरह मिटता है और किस तरह की निरन्तर अतृप्ति उपभोग के बावजूद रहती है और किस तरह यह तृप्ति और अतृप्ति की निरन्तरता एक विराट हाइपर-रीयल को बनाती रहती है इस पर बौद्रीआ ने इस दौर के तमाम अन्य चिन्तकों से ज्यादा काम किया है। वे उस पुस्तक में कहते हैं कि उपभोक्ता संस्कृति में ‘वस्तु’ और उसके ‘प्रतिनिधान’ के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। अन्तर्वस्तु और रूप शैली का फर्क मिट जाता है। यथार्थ की जगह उसकी अनन्त प्रतिच्छवियाँ ले लेती हैं, वे अपने से बाहर किसी सन्दर्भ को रहने नहीं देती। वे अपने में एक यथार्थ होती हैं। यह ‘साइमूलेशन’ ‘उपन्यास’ या ‘कहानी’ के ‘सच’ या ‘झूठ’ से अलग होता है। यह ‘झूठ’ को ‘सच’ ही नहीं बनाता, यह यथार्थ से अपनी समानता सम्बन्ध या तुलना सम्बन्धों को भी मना करता है। यह जगत ‘आत्म सन्दर्भित’ जगत होता है। यह ‘प्रपंच’ का जगत होता है। (ज्यां बौद्रीआ, सलेक्टेड राइटिंग सम्पादक मार्क पॉस्टप पेज 5-6)
यह ‘प्रपंच’, यह साइमूलेशंस, अपने सन्दर्भ की प्रपंची निरन्तरता में प्रायः यथार्थ से भी ज्यादा सच नजर आते हैं। ये पॉपुलर कल्चर में लगातार बनते हैं, जो ‘यथार्थ’ से ‘बेहतर’ नजर आती हैं। यही ‘हाइपर रीयलिज्म’ की विशेषता है जो इन दिनों हर तरफ व्याप्त नजर आती है। लोग टीवी देखकर, सोप ओपेरा देखकर, उनमें बनाए गए चरित्रों के ‘फैन’ बनकर पत्र लिखते हैं, उनसे हमदर्दी रखते हैं जबकि वे यथार्थ में नहीं होते। वे उनसे मिलना चाहते हैं अपने यहाँ। इन दिनों शादियों में लोग डोनाल्ड डक को बुलाते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं। ऐसे अनेक चरित्र जीवन में और जीवन उनमें घुस जाता है जबकि वे ‘यथार्थ’ नहीं होते। बौद्रीआ इस स्थिति को जीवन में टीवी का खपना और टीवी में जीवन का खपना कहते हैं। इसे हम भक्तों में उनके ‘उन्माद’ से देखते हैं, ‘उन्माद’ में भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता दूरी समाप्त कर देता है। पॉपुलर कल्चर उसके माध्यम के यथार्थ और प्रतिनिधान यानी प्रतिबिम्बन के बीच ऐसा ही ‘अ-भेद’ पैदा करती है। पॉपुलर कल्चर इस अभेद को स्थापित करती है।
इस क्रम में ‘पॉपुलर कल्चर’ के प्रगतिशील विद्वान जॉन फिस्के ने अपनी पुस्तक ‘मीडिया मैटर्स’ (1994) में कहा है कि पोस्ट मॉर्डन मीडिया यथार्थ के दोयम प्रतिनिधान नहीं देता। वे उस यथार्थ को बनाते हैं जिसका वे प्रतिनिधान करते हैं। जो भी ‘घटनाएँ’, होती हैं वे ‘मीडिया घटित’ होती हैं। अमेरिका में खिलाड़ी ओ.जे. सिंपसन की गिरफ्तारी इस ‘पॉपुलर कल्चर’ और ‘हाइपर रीयल’ की अन्यतम उदाहरण है। जॉन फिस्के बताते हैं कि किस तरह ‘स्थानीय लोग जो अपने घरों में टीवी पर किसी ‘चेन’ को देख रहे थे वे सब ओ.जे. सिंपसन के घर की ओर चल पड़े। वे अपने साथ अपने पोर्टेबल टीवी सैट ले गए। वे सारी घटना को (सिंपसन की गिरफ्तारी और मुकदमे को, उसके द्वारा किए गए कत्ल की पुनर्रचना को), ‘जीवित’ (लाइव) देखना चाहते थे लेकिन जानते थे कि टीवी पर उसका प्रसारण उस घटना का पूरक है। अपने आपको टीवी पर घटना को देखता देखकर, वे अपने आपको ही हाथ हिलाते थे। पोस्टमॉर्डन मनुष्य को एक साथ इस ही क्षण ‘लाइव पीपल’ और ‘मीडिया पीपल’ बनने में कोई दिक्कत नहीं होती। वे जानते थे कि मीडिया खबर ‘देता’ नहीं है, उसका निर्माण करता है, इसलिए सिंपसन की गिरफ्तारी खबर का हिस्सा बनने के लिए, सिर्फ ‘ऑन द स्पॉट’ होना ही काफी नहीं था उसे टीवी में भी दिखना जरूरी था। पूरा मुकदमा भी इसी तरह ‘दिखा’ ‘बना’ मुकदमा था। वह कोर्ट के लिए उतना नहीं बनाया गया जितना टीवी के लिए बनाया गया था।
अपने टीवी चैनलों पर कैमरे के फ्रेम के भीतर झाँकनेवाले लोगों को याद करें। वे क्यों टीवी में दिखना-होना चाहते हैं ? पॉपुलर होने के लिए कि लोग उन्हें जानें, देखें। इससे उनका ‘पावर’ बढ़ता है। अनेक घटनाएँ कुछ इस तरह की जाने लगी हैं कि वे पॉपुलर होने के लिए उचित उपयुक्त छवि दे सकें, रूप दे सकें। हमारे समाज में इन दिनों ऐसी अनन्त घटनाएँ होती हैं जो जितनी जीवन के लिए होती हैं, उतनी या कभी-कभी उससे ज्यादा टीवी की खातिर की जाती हैं। कोई मीनार पर चढ़ जाता है, कोई डिजाइनर सूट में रहता है, कोई टीवी के लिए सजग होकर बोलता है। सब पॉपुलर होने दिखने के लिए।
इस तरह, ‘पॉपुलर कल्चर’, इस बिन्दु पर आकर ‘आत्मोभोग’ बन जाती है। आप अपने से बाहर ‘पॉपुलर’ नहीं पाते, अपने में ही उसे पाते हैं। छलना में, प्रपंच में जाना, जाने की बढ़ती ललक, स्वयं को सहज यथार्थ से काटकर बनाए यथार्थ में ले आना, बनाए अति चंचल यथार्थ में हिस्सेदार बना लेना नितान्त नया सांस्कृतिक अनुभव एवं बोध है। इसे पोस्ट मॉर्डन भावबोध कहा जा सकता है। यह तो एक उदाहरण है जो यहाँ इसलिए दिया गया है कि टीवी सन्दर्भ सुर्वसुलभ है। उत्तर आधुनिक भावबोध के, पॉपुलर कल्चर में ‘खप’ जाने के अनेक प्रसंग बताए जा सकते हैं।
उत्तर-आधुनिकता और पॉपुलर कल्चर
उत्तर आधुनिकता और पॉप कल्चर अन्योन्याश्रय कही जा सकती हैं।
‘पोस्टमॉर्डर्निज्म एंड पॉपूलर कल्चर’ में जॉन डॉकर
ने लिखा
है कि कुछ वर्ष पहले तक जब टीवी इतना निर्णायक नहीं लगता था तब वामपंथी
बुद्धिजीवी माना करते थे कि टीवी आदि जनता के मनोरंजन का हिस्सा है और
पूँजीपति उसके जरिए अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं।
यह आधुनिकतावादी विमर्श था। जब डॉकर के बच्चा हुआ और वे टीवी कुछ ज्यादा देखने लगे तो लगा कि उक्त आलोचना पूरी तरह ‘ठीक’ नहीं है। तब वे पॉपूलर कल्चर का अध्ययन करने लगे। उत्तर-आधुनिकता के सन्दर्भ में उनके नतीजे कुछ भिन्न ही रहे। उन्होंने पाया कि आधुनिकतावादी नजर से पॉप कल्चर में आलोचनात्मकता की क्षमता नहीं ढूँढ़ी जा सकती। उसे ‘पेस्सिव’ ही माना जाता है। ‘कार्निवाल कल्चर’ दरअसल बूर्ज्वा का वह ‘जनक्षेत्र’ है जिसे वह अपने फैलाव के लिए बनाता है। इसमें वह पहचान के अनेक चिह्न सक्रिय करता है जिनकी परिणतियों पर उसका जोर नहीं होता। पॉप कल्चर अध्ययन का लक्ष्य पॉप कल्चर के निर्माण की प्रक्रिया तो होता ही है उसके उपयोग और परिणतियों को समझना भी होता है।
यह आधुनिकतावादी विमर्श था। जब डॉकर के बच्चा हुआ और वे टीवी कुछ ज्यादा देखने लगे तो लगा कि उक्त आलोचना पूरी तरह ‘ठीक’ नहीं है। तब वे पॉपूलर कल्चर का अध्ययन करने लगे। उत्तर-आधुनिकता के सन्दर्भ में उनके नतीजे कुछ भिन्न ही रहे। उन्होंने पाया कि आधुनिकतावादी नजर से पॉप कल्चर में आलोचनात्मकता की क्षमता नहीं ढूँढ़ी जा सकती। उसे ‘पेस्सिव’ ही माना जाता है। ‘कार्निवाल कल्चर’ दरअसल बूर्ज्वा का वह ‘जनक्षेत्र’ है जिसे वह अपने फैलाव के लिए बनाता है। इसमें वह पहचान के अनेक चिह्न सक्रिय करता है जिनकी परिणतियों पर उसका जोर नहीं होता। पॉप कल्चर अध्ययन का लक्ष्य पॉप कल्चर के निर्माण की प्रक्रिया तो होता ही है उसके उपयोग और परिणतियों को समझना भी होता है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i