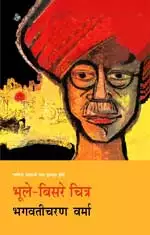|
समाजवादी >> भूले बिसरे चित्र भूले बिसरे चित्रभगवतीचरण वर्मा
|
420 पाठक हैं |
|||||||
संयुक्त परिवार-प्रथा का विघटन, सामंतवाद की पूँजीवाद द्वारा पराजय, व मध्यवर्ग का उदय राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलन का विकास इन चार बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है......
Bhule Bisre Chitra a hindi book by Bhagwati Charan Verma - भूले बिसरे चित्र - भगवतीचरण वर्मा
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भूले-बिसरे चित्र मूलतः एक महाकाव्य उपन्यास है। डिमाई 440 पृष्टों के इस उपन्यास का यह संक्षिप्त संस्करण है। मूल आधिकारिक कथा के विकास को ध्यान में रखकर ही इसे संक्षिप्त किया गया है, इससे यह उपन्यास अधिक सुगठित स्पष्ट एवं कलात्मक हो गया है ।
संयुक्त परिवार-प्रथा का विघटन, मध्यवर्ग के उदय, सामंवतवाद की पूँजी द्वारा पराजय तथा राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-आंदोलन का विकास ये चार आधार बिन्दु हैं, जिस पर इस उपन्यास का कथानक खड़ा होता है। इन्हीं चारों की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया के माध्यम से उपन्यास की सम्पूर्ण अंतर्योजना गठित होती है। कथाकाल् सन् 1880 से 1930 तक फैला हुआ है। इसे एक प्रकार का ‘पीरियड नावेल’ कहा जा सकता है।
उपन्यास की भाषा में बोलचाल का वही सहज-सरल स्वर है जो हमें प्रेमचन्द्र में मिलता है। लेखक ने आलंकारिकता या अतिरिक्त भावुकता से भरी भाषा का प्रयोग न करके भाषा के जिस गठन और लहजे को स्वीकार किया है, वह उपन्यास को अधिक रोचक और सार्थक बनाता है। वस्तुतः इस उपन्यास में जिस अर्द्धशती के भूले-बिसरे चित्रों को पुनः याद के सहारे अंकित किया गया है, वे अपनी रोचकता में हमें आकर्षित करते हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी साहित्य की एक कृति है-भूले-बिसरे चित्र अपने ढंग से प्रेरक भी है और ज्ञानवर्द्धक भी।
संयुक्त परिवार-प्रथा का विघटन, मध्यवर्ग के उदय, सामंवतवाद की पूँजी द्वारा पराजय तथा राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-आंदोलन का विकास ये चार आधार बिन्दु हैं, जिस पर इस उपन्यास का कथानक खड़ा होता है। इन्हीं चारों की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया के माध्यम से उपन्यास की सम्पूर्ण अंतर्योजना गठित होती है। कथाकाल् सन् 1880 से 1930 तक फैला हुआ है। इसे एक प्रकार का ‘पीरियड नावेल’ कहा जा सकता है।
उपन्यास की भाषा में बोलचाल का वही सहज-सरल स्वर है जो हमें प्रेमचन्द्र में मिलता है। लेखक ने आलंकारिकता या अतिरिक्त भावुकता से भरी भाषा का प्रयोग न करके भाषा के जिस गठन और लहजे को स्वीकार किया है, वह उपन्यास को अधिक रोचक और सार्थक बनाता है। वस्तुतः इस उपन्यास में जिस अर्द्धशती के भूले-बिसरे चित्रों को पुनः याद के सहारे अंकित किया गया है, वे अपनी रोचकता में हमें आकर्षित करते हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी साहित्य की एक कृति है-भूले-बिसरे चित्र अपने ढंग से प्रेरक भी है और ज्ञानवर्द्धक भी।
सतर्क अध्ययन के लिए
एक मोटा सोंटा था और उस पर यह खुदा हुआ था कि सोंटा सबको तोड़ता है। यह डण्डा था फ्रांस के 19 वीं शती के प्रसिद्ध उपन्यासकार हेनरी बाल्ज़क का। 20 वीं शती के जर्मन उपन्यासकार फ्रेंज काफ़्का ने जब इस सोंटे की कथा सुनी तो एक छोटी-सी छड़ी पर यह खुदवाया कि इस छड़ी को हर चीज तोड़ती है। आलोचकों का कहना है कि ये दो प्रतीक हैं- यूरोपीय उपन्यास की विकास-यात्रा के। बाल्ज़क का उपन्यास ही वह सोंटा था जिससे वे अपने युग की हर अशुचि, रूढ़ि एवं विकृति तोड़ रहे थे। वस्तुत: उपन्यास नामक साहित्य का यह कथा-रूप सचेत मध्यवर्ग की साहित्यिक अभिव्यंजना होने के कारण प्रारम्भ से समाज एवं मनुष्य की पारस्परिक स्थितियों, द्वन्दों, समस्याओं आदि की ओर उन्मुख रहा है। इसे सर्वेण्टीज़ में देखा जा सकता है और सौभाग्य से हिन्दी के पहले उपन्यास ‘परीक्षागुरु’ (लाला श्रीनिवासदास) में भी यह जागरूकता विद्यमान है।
कथा-कहानी मनोरंजन के लिए ही नहीं, उपदेश के लिए पहले भी प्रयुक्त होती रही हैं। पर आधुनिक जीवन की क्षमताओं को स्वीकार कर यथार्थ की भूमि पर विविध सामाजिक संबंधों के परिदृश्य में समस्याओं को समझने-बूझने और झाँकने का प्रयत्न इस आधुनिक कथा-रूप में ही सम्भव हो सका है। पढ़ने में मज़ा (मनोरंजकता) तो मिलता ही रहा, पर गढ़े-गढ़ाए उपदेशों के स्थान पर यह समस्यामूलकता उसकी एक बड़ी शक्ति है जो लेखक की जागरूकता, प्रबुद्धता और निरीक्षण-शक्ति का परिचय देती है। सजीव पात्र-योजना, विश्वसनीय घटनावली और परिस्थितियाँ जिस आधार-बिन्दु (थीम) पर नाना प्रकार की विधियों से वर्णित-चित्रित होते हैं, वह उपन्यास को पुराने कथा-रूपों से एकदम अलग कर देता है। ‘फिर क्या हुआ’ से आगे बढ़कर ‘क्यों हुआ’ ? ‘क्या हो रहा है ?’ और ‘क्या होगा ?’ जैसे प्रश्न प्रमुख हो गए। कहना न होगा कि इनमें भी आधार भूत प्रश्न मध्यवर्ती ही है।
अस्तु, हिन्दी-उपन्यास प्रारम्भ से ही आधुनिकता के उस बीज को स्वीकार करता है। जिन रूढ़ियों, अशुचिताओं एवं विकृतियों पर भारतेन्दु या प्रतापनारायण अपने नाटकों या निबंधों से प्रहार कर रहे थे, उन्हीं पर लाला श्रीनिवासदास या बालकृष्ण भट्ट अपने उपन्यासों को पैना कर रहे थे। समस्याओं को समझने और जूझने की वही आकांक्षा है। यह बात शायद कुछ विचित्र-सी लगे, पर सचाई यह है कि ‘चन्द्रकान्ता सन्तति’ की तमाम अतिरंजनाओं एवं चमत्कारों के मूल में यही मानवीय, लौकिक, यथार्थवादी दृष्टि है जो ढहते हुए सामन्तवाद एवं नवोदित पूँजीवाद को प्रतीक अथवा ‘फेण्टेसी’ की भाषा में उपस्थित कर रही थी।
भारतेन्दु-युग के उस प्रारम्भिक उपन्यास की सराहना करते हुए भी एक बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि यह दृष्टि बहुत-कुछ स्थूल है। पात्रों एवं घटनाओं के उपादानों को एक व्यवस्थित रूपाकार में ढाला भी नहीं जा सका है। समस्याओं के अनुरूप चरित्रों एवं घटनाओं के साँचे गढ़ लिए गए हैं। यथार्थ की सूक्ष्म-निरीक्षिणी दृष्टि का अभाव था। यह प्रभाव प्रेमचन्द्र द्वारा भरा गया है। उनके उपन्यासों में समस्याएँ सीधे उपन्यासों में उगती हैं। प्रेमचन्द की वास्तविक खोज समस्याओं के समाधान की नहीं है (वह ऊपरी और आरोपित है, इसलिए अकलात्मक भी), बल्कि उपन्यास के लिए चरित्र, परिस्थिति, गठन एवं इन सबसे ऊपर एक उपयुक्त भाषा की खोज है। गहरी यथार्थ-दृष्टि, व्यापक मानवीय संवेदना, किस्सागो की आत्मीयता एवं भाषा का अत्यन्त सृजनात्मक प्रयोग प्रेमचन्द की विशिष्ट क्षमताएँ हैं। उनके उपन्यास वैयक्तिक संवेदना एवं सामाजिक इतिहास के मिलन-बिन्दु ही नहीं हैं, चौराहे भी हैं। उनके उपन्यासों में व्यक्ति प्रमुख है या समाज-इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट ‘हाँ’ या ‘ना’ में नहीं दिया जा सकता। जहाँ वे एक-दूसरे को पार करते हैं, काटते हैं, उसी बिन्दु पर उनके उपन्यासों का सारा ढाँचा खड़ा होता है। प्रेमचन्द का मनोविज्ञान भी सहज एवं दैनिक व्यवहार का है। एक प्रकार का अपराजेय संकल्प एवं दुर्दम विश्वास उनके प्रारम्भिक उपन्यासों में मिलता है, जो राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रथम चरण के आशावाद एवं विश्वास का प्रतीक भी है। पर सन् 1930 तक पहुँचते-पहुँचते आन्दोलन की असफलताएँ प्रबुद्ध मानस को पीड़ित भी करने लगी थीं और ईमानदार कलाकार की संपूर्ण सचाई के साथ प्रेमचन्द्र इस कटु यथार्थ को भी सामने लाते हैं।
पराजय, असफलता एवं निराशा से व्याप्त राष्ट्रीय वातावरण में ही 1930 के आसपास के लेखकों की एक और नयी पीढी़ सामने आती है। 19 वीं शती में जिस मध्यवर्ग का उदय हुआ था, वह भी अब अपना स्वरूप ही नहीं, नियति भी पहचानने लगा था। इधर देश में शिक्षा, उद्योग, विज्ञान आदि के प्रसार के साथ-साथ प्रबुद्धता एवं विशेषीकरण की स्थिति भी वर्द्धमान थी। मार्क्स, फ्रायड और डार्विन, सभी वातावरण के सघन बना रहे थे। इन विचारकों ने मनुष्य की अब तक की बद्धमूल एवं युगसिद्ध मान्यताओं को आमूलचूल हिला दिया था। इसी प्रकार के वैद्युतिक आवेश के वातावरण में तीसी की यह पीढ़ी उठ रही थी। एक ओर इनके भीतर मध्यवर्ग का व्यक्तिवादी-स्वच्छन्दतावादी दर्शन था और दूसरी ओर प्रत्यक्ष जीवन में (चाहे प्रेम का क्षेत्र हो या राजनीति का) निरन्तर असफलता का अनुभव हो रहा था। इनका क्षुब्ध अहं। घूम-फिरकर परिस्थितियों को दोष दे रहा था। नवीन विचारों के आलोक में नीति-अनीति, पाप-पुण्य, प्रेम-वासना को भी ये लेखक पुन: विवेचित कर लेना चाहते थे। इन लेखकों में यदि कुछ लेखक व्यापक समाज से कटे हुए व्यक्ति के मन की अनथाही गहराइयों को नापना चाहते हैं, तो कुछ तेजी से बदल रहे एवं अन्तत: पराजय की ओर बढ़ रहे जीवन का हर क्षण भोग लेना चाहते हैं। जीवन को भोग लेने की इस आकुलता में ही अकसर नीति-अनीति, पाप-पुण्य के प्रश्न उनके सामने उभरते हैं। तथा कुछ लोग घबराकर सब-कुछ नष्ट कर देने वाला हिंसक और अराजकतावादी दर्शन अपनाने को भी विवश होते हैं।
तीसी की इस पीढ़ी के ही एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि भगवतीचरण वर्मा हैं। वे उस समय की तरुण पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जिसे एक ओर जीवन का ज्वार लहरों से खेलने के लिए आमन्त्रित करता है और दूसरी ओर उसकी विशालता से अभिभूत ये अपना नाश भी निश्चित-सा मानते हैं। उन लोगों का अकेला अहं क्षुब्ध होकर यह अनुभव करता है कि देश और काल में फैला यह ज्वार उनसे बड़ा है। सामाजिक जीवन से हारे हुए व्यक्ति की वेदना की महिमा के गीत ही उस काल के तमाम साहित्य-रूपों में गाये गए हैं। इसके अपवाद न बँगला के शरतचन्द्र है, और न हिन्दी के जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी या भगवतीचरण वर्मा। ‘बच्चन’, ‘अंचल’ या नरेन्द्र शर्मा के गीतों की भी यही पृष्ठभूमि है। पर इतना ध्यान में रखना होगा कि इस पराजयाक्रान्ति में भी विद्रोह का क्षुब्ध स्वर बराबर बना रहा है-भले ही वह विद्रोह अन्तत: निष्फल ही क्यों न मालूम पड़े।
इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर पढ़ने से भगवतीचरण वर्मा के उपन्यासों का अर्थ और प्रतीकता अधिक स्पष्ट रूप में सामने आती है। ‘चित्रलेखा’, ‘तीन वर्ष’ एवं ‘टेढ़े-मेढ़े रास्ते’ उनके इन तीन प्रारम्भिक उपन्यासों के मुख्य पात्र विशिष्ट, वैयक्ति अहं से मण्डित हैं और प्रत्येक किसी-न-किसी बिन्दु पर असफल होता नज़र आता है। ‘चित्रलेखा’ में अतीत के फलक पर पाप-पुण्य की समस्या है, ‘तीन वर्ष’ में वर्तमान के धरातल पर विवाह, प्रेम और वासना का प्रश्न है तथा ‘टेढ़े-मेढ़े रास्ते’ में समसामयिक राजनीति विश्वासों के आगे प्रश्नचिह्न हैं। सर्वत्र मूल में एक ही विचारधारा है कि ‘मनुष्य परिस्थितियों का दास है’। पूर्वग्रहीत मान्यताओं पर सर्वत्र एक ठोकर है : न कोई पापी है, न पुण्यात्मा, कुलकन्या से श्रेष्ठतर वेश्या हो सकती है और सारे राजनीतिक विश्वास झूठे हैं। इसे एक प्रकार की क्षयी जीनव-दर्शन भी कहा जा सकता है, जोकि यही दर्शन उस समय के व्यक्ति को बल देता है। 1959 ई. में प्रकाशित ‘भूले बिसरे चित्र’ में ज्वालाप्रसाद भी यही कहकर अपने मन को हल्का करते हैं : ‘मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, बिलकुल कुछ नहीं है, फिर चिन्ता किस बात की जाए ? जो होना है, वह हो चुका है, उसे रोका नहीं जा सकता।’ (पृष्ठ 334: प्रस्तुत संस्करण)
अपनी पीढ़ी के समसामयिक उपन्याकारों के मध्य भगवती बाबू एक अर्थ में नितान्त हैं कि जब जैनेन्द्र या इलाचन्द्र जोशी अधिकाधिक व्यक्ति-मन के विश्लेषण में लगे थे तब भी वे सामाजिक यथार्थ में संलग्न रहे। उनके चित्रण का कैनवास प्रेमचन्द्र-जैसा व्यापक तो नहीं है, पर मध्यवर्ग के विविध संबंधों के तनावों और क्रिया-प्रतिक्रियाओं के बीच अपने पात्रों एवं समस्याओं को उन्होंने उभारा है। उनके उपन्यासों का मूल ढाँचा बहुधा परिवार-केन्द्रित है। इस संदर्भ में वे प्रेमचन्द की परंपरा के अपेक्षाकृत अधिक निकट रहे। तथा कहने की रोचकता भी उनमें प्रेमचन्द-जैसी ही थी-अपने समकालीन उपन्यासकारों से कहीं अधिक। एक और तथ्य भी द्रष्टव्य है कि विचार और दर्शन की ओर उनका झुकाव कम होता गया है, जबकि अन्य उपन्यासकारों में यह व्याधि बढ़ी है। शायद जिस दर्शन को भगवती बाबू ने अपनाया है उसकी सम्भावित परिणति घटना-बहुलता ही है।
ऊपर विवेचित पहले के तीनों उपन्यासों के बाद भगवती बाबू की कला में कुछ गिराव आया था। ‘आखिरी दाँव’ उनकी अपेक्षाकृत कमजोर उपन्यास है। परन्तु पुन: ‘भूले बिखरे चित्र’ तथा ‘सामर्थ्य और सीमा’ में उन्होंने पर्याप्त शक्ति और कौशल का प्रमाण दिया है। ‘भूले बिखरे चित्र’ पर तो उन्हें ‘साहित्य अकादमी’ एवं ‘हिन्दुस्तानी एकेडमी’ के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
कथा-कहानी मनोरंजन के लिए ही नहीं, उपदेश के लिए पहले भी प्रयुक्त होती रही हैं। पर आधुनिक जीवन की क्षमताओं को स्वीकार कर यथार्थ की भूमि पर विविध सामाजिक संबंधों के परिदृश्य में समस्याओं को समझने-बूझने और झाँकने का प्रयत्न इस आधुनिक कथा-रूप में ही सम्भव हो सका है। पढ़ने में मज़ा (मनोरंजकता) तो मिलता ही रहा, पर गढ़े-गढ़ाए उपदेशों के स्थान पर यह समस्यामूलकता उसकी एक बड़ी शक्ति है जो लेखक की जागरूकता, प्रबुद्धता और निरीक्षण-शक्ति का परिचय देती है। सजीव पात्र-योजना, विश्वसनीय घटनावली और परिस्थितियाँ जिस आधार-बिन्दु (थीम) पर नाना प्रकार की विधियों से वर्णित-चित्रित होते हैं, वह उपन्यास को पुराने कथा-रूपों से एकदम अलग कर देता है। ‘फिर क्या हुआ’ से आगे बढ़कर ‘क्यों हुआ’ ? ‘क्या हो रहा है ?’ और ‘क्या होगा ?’ जैसे प्रश्न प्रमुख हो गए। कहना न होगा कि इनमें भी आधार भूत प्रश्न मध्यवर्ती ही है।
अस्तु, हिन्दी-उपन्यास प्रारम्भ से ही आधुनिकता के उस बीज को स्वीकार करता है। जिन रूढ़ियों, अशुचिताओं एवं विकृतियों पर भारतेन्दु या प्रतापनारायण अपने नाटकों या निबंधों से प्रहार कर रहे थे, उन्हीं पर लाला श्रीनिवासदास या बालकृष्ण भट्ट अपने उपन्यासों को पैना कर रहे थे। समस्याओं को समझने और जूझने की वही आकांक्षा है। यह बात शायद कुछ विचित्र-सी लगे, पर सचाई यह है कि ‘चन्द्रकान्ता सन्तति’ की तमाम अतिरंजनाओं एवं चमत्कारों के मूल में यही मानवीय, लौकिक, यथार्थवादी दृष्टि है जो ढहते हुए सामन्तवाद एवं नवोदित पूँजीवाद को प्रतीक अथवा ‘फेण्टेसी’ की भाषा में उपस्थित कर रही थी।
भारतेन्दु-युग के उस प्रारम्भिक उपन्यास की सराहना करते हुए भी एक बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि यह दृष्टि बहुत-कुछ स्थूल है। पात्रों एवं घटनाओं के उपादानों को एक व्यवस्थित रूपाकार में ढाला भी नहीं जा सका है। समस्याओं के अनुरूप चरित्रों एवं घटनाओं के साँचे गढ़ लिए गए हैं। यथार्थ की सूक्ष्म-निरीक्षिणी दृष्टि का अभाव था। यह प्रभाव प्रेमचन्द्र द्वारा भरा गया है। उनके उपन्यासों में समस्याएँ सीधे उपन्यासों में उगती हैं। प्रेमचन्द की वास्तविक खोज समस्याओं के समाधान की नहीं है (वह ऊपरी और आरोपित है, इसलिए अकलात्मक भी), बल्कि उपन्यास के लिए चरित्र, परिस्थिति, गठन एवं इन सबसे ऊपर एक उपयुक्त भाषा की खोज है। गहरी यथार्थ-दृष्टि, व्यापक मानवीय संवेदना, किस्सागो की आत्मीयता एवं भाषा का अत्यन्त सृजनात्मक प्रयोग प्रेमचन्द की विशिष्ट क्षमताएँ हैं। उनके उपन्यास वैयक्तिक संवेदना एवं सामाजिक इतिहास के मिलन-बिन्दु ही नहीं हैं, चौराहे भी हैं। उनके उपन्यासों में व्यक्ति प्रमुख है या समाज-इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट ‘हाँ’ या ‘ना’ में नहीं दिया जा सकता। जहाँ वे एक-दूसरे को पार करते हैं, काटते हैं, उसी बिन्दु पर उनके उपन्यासों का सारा ढाँचा खड़ा होता है। प्रेमचन्द का मनोविज्ञान भी सहज एवं दैनिक व्यवहार का है। एक प्रकार का अपराजेय संकल्प एवं दुर्दम विश्वास उनके प्रारम्भिक उपन्यासों में मिलता है, जो राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रथम चरण के आशावाद एवं विश्वास का प्रतीक भी है। पर सन् 1930 तक पहुँचते-पहुँचते आन्दोलन की असफलताएँ प्रबुद्ध मानस को पीड़ित भी करने लगी थीं और ईमानदार कलाकार की संपूर्ण सचाई के साथ प्रेमचन्द्र इस कटु यथार्थ को भी सामने लाते हैं।
पराजय, असफलता एवं निराशा से व्याप्त राष्ट्रीय वातावरण में ही 1930 के आसपास के लेखकों की एक और नयी पीढी़ सामने आती है। 19 वीं शती में जिस मध्यवर्ग का उदय हुआ था, वह भी अब अपना स्वरूप ही नहीं, नियति भी पहचानने लगा था। इधर देश में शिक्षा, उद्योग, विज्ञान आदि के प्रसार के साथ-साथ प्रबुद्धता एवं विशेषीकरण की स्थिति भी वर्द्धमान थी। मार्क्स, फ्रायड और डार्विन, सभी वातावरण के सघन बना रहे थे। इन विचारकों ने मनुष्य की अब तक की बद्धमूल एवं युगसिद्ध मान्यताओं को आमूलचूल हिला दिया था। इसी प्रकार के वैद्युतिक आवेश के वातावरण में तीसी की यह पीढ़ी उठ रही थी। एक ओर इनके भीतर मध्यवर्ग का व्यक्तिवादी-स्वच्छन्दतावादी दर्शन था और दूसरी ओर प्रत्यक्ष जीवन में (चाहे प्रेम का क्षेत्र हो या राजनीति का) निरन्तर असफलता का अनुभव हो रहा था। इनका क्षुब्ध अहं। घूम-फिरकर परिस्थितियों को दोष दे रहा था। नवीन विचारों के आलोक में नीति-अनीति, पाप-पुण्य, प्रेम-वासना को भी ये लेखक पुन: विवेचित कर लेना चाहते थे। इन लेखकों में यदि कुछ लेखक व्यापक समाज से कटे हुए व्यक्ति के मन की अनथाही गहराइयों को नापना चाहते हैं, तो कुछ तेजी से बदल रहे एवं अन्तत: पराजय की ओर बढ़ रहे जीवन का हर क्षण भोग लेना चाहते हैं। जीवन को भोग लेने की इस आकुलता में ही अकसर नीति-अनीति, पाप-पुण्य के प्रश्न उनके सामने उभरते हैं। तथा कुछ लोग घबराकर सब-कुछ नष्ट कर देने वाला हिंसक और अराजकतावादी दर्शन अपनाने को भी विवश होते हैं।
तीसी की इस पीढ़ी के ही एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि भगवतीचरण वर्मा हैं। वे उस समय की तरुण पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जिसे एक ओर जीवन का ज्वार लहरों से खेलने के लिए आमन्त्रित करता है और दूसरी ओर उसकी विशालता से अभिभूत ये अपना नाश भी निश्चित-सा मानते हैं। उन लोगों का अकेला अहं क्षुब्ध होकर यह अनुभव करता है कि देश और काल में फैला यह ज्वार उनसे बड़ा है। सामाजिक जीवन से हारे हुए व्यक्ति की वेदना की महिमा के गीत ही उस काल के तमाम साहित्य-रूपों में गाये गए हैं। इसके अपवाद न बँगला के शरतचन्द्र है, और न हिन्दी के जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी या भगवतीचरण वर्मा। ‘बच्चन’, ‘अंचल’ या नरेन्द्र शर्मा के गीतों की भी यही पृष्ठभूमि है। पर इतना ध्यान में रखना होगा कि इस पराजयाक्रान्ति में भी विद्रोह का क्षुब्ध स्वर बराबर बना रहा है-भले ही वह विद्रोह अन्तत: निष्फल ही क्यों न मालूम पड़े।
इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर पढ़ने से भगवतीचरण वर्मा के उपन्यासों का अर्थ और प्रतीकता अधिक स्पष्ट रूप में सामने आती है। ‘चित्रलेखा’, ‘तीन वर्ष’ एवं ‘टेढ़े-मेढ़े रास्ते’ उनके इन तीन प्रारम्भिक उपन्यासों के मुख्य पात्र विशिष्ट, वैयक्ति अहं से मण्डित हैं और प्रत्येक किसी-न-किसी बिन्दु पर असफल होता नज़र आता है। ‘चित्रलेखा’ में अतीत के फलक पर पाप-पुण्य की समस्या है, ‘तीन वर्ष’ में वर्तमान के धरातल पर विवाह, प्रेम और वासना का प्रश्न है तथा ‘टेढ़े-मेढ़े रास्ते’ में समसामयिक राजनीति विश्वासों के आगे प्रश्नचिह्न हैं। सर्वत्र मूल में एक ही विचारधारा है कि ‘मनुष्य परिस्थितियों का दास है’। पूर्वग्रहीत मान्यताओं पर सर्वत्र एक ठोकर है : न कोई पापी है, न पुण्यात्मा, कुलकन्या से श्रेष्ठतर वेश्या हो सकती है और सारे राजनीतिक विश्वास झूठे हैं। इसे एक प्रकार की क्षयी जीनव-दर्शन भी कहा जा सकता है, जोकि यही दर्शन उस समय के व्यक्ति को बल देता है। 1959 ई. में प्रकाशित ‘भूले बिसरे चित्र’ में ज्वालाप्रसाद भी यही कहकर अपने मन को हल्का करते हैं : ‘मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, बिलकुल कुछ नहीं है, फिर चिन्ता किस बात की जाए ? जो होना है, वह हो चुका है, उसे रोका नहीं जा सकता।’ (पृष्ठ 334: प्रस्तुत संस्करण)
अपनी पीढ़ी के समसामयिक उपन्याकारों के मध्य भगवती बाबू एक अर्थ में नितान्त हैं कि जब जैनेन्द्र या इलाचन्द्र जोशी अधिकाधिक व्यक्ति-मन के विश्लेषण में लगे थे तब भी वे सामाजिक यथार्थ में संलग्न रहे। उनके चित्रण का कैनवास प्रेमचन्द्र-जैसा व्यापक तो नहीं है, पर मध्यवर्ग के विविध संबंधों के तनावों और क्रिया-प्रतिक्रियाओं के बीच अपने पात्रों एवं समस्याओं को उन्होंने उभारा है। उनके उपन्यासों का मूल ढाँचा बहुधा परिवार-केन्द्रित है। इस संदर्भ में वे प्रेमचन्द की परंपरा के अपेक्षाकृत अधिक निकट रहे। तथा कहने की रोचकता भी उनमें प्रेमचन्द-जैसी ही थी-अपने समकालीन उपन्यासकारों से कहीं अधिक। एक और तथ्य भी द्रष्टव्य है कि विचार और दर्शन की ओर उनका झुकाव कम होता गया है, जबकि अन्य उपन्यासकारों में यह व्याधि बढ़ी है। शायद जिस दर्शन को भगवती बाबू ने अपनाया है उसकी सम्भावित परिणति घटना-बहुलता ही है।
ऊपर विवेचित पहले के तीनों उपन्यासों के बाद भगवती बाबू की कला में कुछ गिराव आया था। ‘आखिरी दाँव’ उनकी अपेक्षाकृत कमजोर उपन्यास है। परन्तु पुन: ‘भूले बिखरे चित्र’ तथा ‘सामर्थ्य और सीमा’ में उन्होंने पर्याप्त शक्ति और कौशल का प्रमाण दिया है। ‘भूले बिखरे चित्र’ पर तो उन्हें ‘साहित्य अकादमी’ एवं ‘हिन्दुस्तानी एकेडमी’ के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i