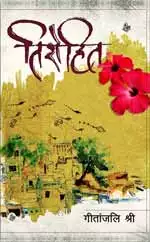|
नारी विमर्श >> तिरोहित तिरोहितगीतांजलि श्री
|
135 पाठक हैं |
|||||||
इसमें स्त्रियों के घरेलू जीवन की अनुभूतियों,रोजमर्रा के स्वाद,स्पर्श,महक,दृश्य को बड़ी बारीकी से उकेरा गया है.....
Tirohit
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
गीतांजलि श्री के लेखन में अमूमन, और तिरोहित में ख़ास तौर से, सब कुछ ऐसा अप्रकट ढंग से घटता है कि पाठक ठहर-से जाते हैं। जो कुछ मारके का है, जीवन को बदल देने वाला है, उपन्यास के फ्रेम के बाहर होता है। ज़िन्दगियाँ चलती-बदलती हैं, नए-नए राग-द्वेष उभरते हैं, प्रतिदान और प्रतिशोध होते हैं, पर चुपके-चुपके। व्यक्त से अधिक मुखर होता है अनकहा। घटनाक्रम के बजाय केन्द्र में रहती हैं चरित्र-चित्रण व पात्रों के आपसी रिश्तों की बारीकियाँ।
पैनी तराशी हुई गद्य शैली, विलक्षण बिम्बसृष्टि और दो चरित्रों-ललना और भतीजा-के परस्पर टकराते स्मृति प्रवाह के सहारे उद्घाटित होते हैं तिरोहित के पात्र उनकी मनोगत इच्छाएँ, वासनाएँ व जीवन से किए गए किन्तु रीते रह गए उनके दावे।
अन्दर-बाहर की अदला-बदली को चरितार्थ करती यहाँ तिरती रहती है एक रहस्यमयी छत। मुहल्ले के तमाम घरों को जोड़ती यह विशाल खुली सार्वजनिक जगह बार-बार भर जाती है चच्चो और ललना के अन्तर्मन के घेरों से। इसी से बनता है कथानक का रूप। जो हमें दिखाता है चच्चो/बहनजी और ललना की इच्छाओं और उनके जीवन की परिस्थितियों के बीच न पट सकने वाली दूरी। वैसी ही दूरी रहती है इन स्त्रियों के स्वयं भोगे यथार्थ और समाज द्वारा देखी गई उनकी असलियत में। निरन्तर तिरोहित होती रहती हैं वे समाज के देखे जाने में।
किन्तु चच्चो/बहनजी और ललना अपने अन्तर्द्वन्द्वों और संघर्षों का सामना भी करती हैं। उस अपार सीधे-सच्चे साहस से जो सामान्य ज़िन्दगियों का स्वभाव बन जाता है।
गीतांजलि श्री ने इन स्त्रियों के घरेलू जीवन की अनुभूतियों रोजमर्रा के स्वाद, स्पर्श, महक, दृश्य-को बड़ी बारीकी से उनकी पूरी सैन्सुअलिटी में उकेरा है।
मौत के तले चलते यादों के सिलसिले में छाया रहता है निविड़ दुःख। अतीत चूँकि बीतता नहीं, यादों के सहारे अपने जीवन का अर्थ पाने वाले तिरोहित के चरित्र-ललना और भजीता अविभाज्य हो जाते हैं दिवंगत चच्चो से। और चच्चो स्वयं रूप लेती हैं इन्हीं यादों में।
पैनी तराशी हुई गद्य शैली, विलक्षण बिम्बसृष्टि और दो चरित्रों-ललना और भतीजा-के परस्पर टकराते स्मृति प्रवाह के सहारे उद्घाटित होते हैं तिरोहित के पात्र उनकी मनोगत इच्छाएँ, वासनाएँ व जीवन से किए गए किन्तु रीते रह गए उनके दावे।
अन्दर-बाहर की अदला-बदली को चरितार्थ करती यहाँ तिरती रहती है एक रहस्यमयी छत। मुहल्ले के तमाम घरों को जोड़ती यह विशाल खुली सार्वजनिक जगह बार-बार भर जाती है चच्चो और ललना के अन्तर्मन के घेरों से। इसी से बनता है कथानक का रूप। जो हमें दिखाता है चच्चो/बहनजी और ललना की इच्छाओं और उनके जीवन की परिस्थितियों के बीच न पट सकने वाली दूरी। वैसी ही दूरी रहती है इन स्त्रियों के स्वयं भोगे यथार्थ और समाज द्वारा देखी गई उनकी असलियत में। निरन्तर तिरोहित होती रहती हैं वे समाज के देखे जाने में।
किन्तु चच्चो/बहनजी और ललना अपने अन्तर्द्वन्द्वों और संघर्षों का सामना भी करती हैं। उस अपार सीधे-सच्चे साहस से जो सामान्य ज़िन्दगियों का स्वभाव बन जाता है।
गीतांजलि श्री ने इन स्त्रियों के घरेलू जीवन की अनुभूतियों रोजमर्रा के स्वाद, स्पर्श, महक, दृश्य-को बड़ी बारीकी से उनकी पूरी सैन्सुअलिटी में उकेरा है।
मौत के तले चलते यादों के सिलसिले में छाया रहता है निविड़ दुःख। अतीत चूँकि बीतता नहीं, यादों के सहारे अपने जीवन का अर्थ पाने वाले तिरोहित के चरित्र-ललना और भजीता अविभाज्य हो जाते हैं दिवंगत चच्चो से। और चच्चो स्वयं रूप लेती हैं इन्हीं यादों में।
-अनुराधा कपूर
किसी की काया को वह नहीं समझो। नम्य निरिंग उस काया के आगे-आगे जो अदृश्य भूत चलती, उसे देखा तुमने ? छत पर, बहन जी के सधे पाँव के आगे पड़ता उसका छनक-मनक पाँव ? पीछे-पीछे काया चलती, आगे-आगे वह अदृश्य दौड़ती। अँधेरों में बहन जी मेरा हाथ पकड़कर दौड़ी तो वह उसकी काया के आगेवाली-और तेज़ दौड़ी ! निरन्तर उससे आगे। अतिलिप्सा से भरी, कभी अपने में काफ़ी नहीं, हमेशा उससे ज़्यादा की चाह, अपनी ही खाल को फाड़ के निकलती !
-इसी पुस्तक से
दीवारों के कान ज़रूर होते हैं पर अफ़सोस, इस छत के नीचे रहनेवालों को अफसोस था कि उनकी ज़ुबान नहीं होती, नहीं तो इन घरों की दीवारें कितनी कहानियाँ सुना सकती थीं, मोहल्ले के अन्दर के पोशीदा पलों की। कहानियाँ सुनाने को इंसान रह गए जिनकी, दीवारों के विपरीत, ज़ुबान तो बहुत थी पर कान ज़रा कम। और आँख और भी कम। जो कमियाँ मगर, ज़ुबान के रहते आड़े नहीं आतीं-कहानियाँ कही भी जाने लगती हैं, गढ़ी भी जाने लगती हैं, सच होती भी जाने लगती हैं ! छत पर पेंग बढ़ाती हवा में गूँजने लगती हैं, रोशनदानों में मकड़ी के बुने सतरंगी जालों के पार दिखाई भी दे जाती हैं।
इसी छत की बात है-कि मोहल्ले के बच्चे एक दूसरे की नकल-नकलाई में पड़ और बालिगों की कही-सुनाई पे उछल इक्कड़-दुक्कड़ खेलते-खेलते नाहक बीच में टाइम्स चिल्ला देते और दौड़ जाते इस घर के रोशनदान से नीचे झाँकने और नर्वस सी खिलखिलाई शुरू करने। मैं खुद उनके साथ दौड़ जाता और कमरे में झाँकने लगता और मुझसे बड़े बच्चे पकड़ते मेरी निकर और धमकाते-
बोल देखा न जो हमने देखा,
ढन ढन ढन ढन होते देखा !
तो मैं कसके निकर को ऊपर खींचे रखता और उन्हें खुश करने को चिल्लाता-
देखा मैंने ढन ढन देखा।
ढन ढन पर सिर मज़े से डुलाता जिस पर सबके साथ मैं भी हँस देता और वापस गुट्टी फेंककर एक पैर पर कूदने लगता।
बड़े लेकिन, झाँकने के बाद, इक्कड़-दुक्कड़ नहीं खेलते। रोशनदान का एन्शेन्ट धूमिल-धूसरित चटका शीशा वह जादू के चश्मे का शीशा था जिसके पार से आकर कहानियाँ हिंडोला बन जातीं और इस छत पर ढेंरों पूरे वयस्क लोग बस झूलते जाते, मचल-मचल जाते, मोहल्ले भर की हवा में ऊँची-ऊँची पेंगों की फूँक भर देते।
देख लिया न, वह पूछते। बच्चों ने भी तो यही देखा, बच्चे तो झूठ नहीं बोलते, बच्चे तो मन के सच्चे हैं न, नहीं, वह अपने विश्वास की दीवार बनाते। रोशनदान से नीचे झाँका तो यही न देखा कि चाचा और ललना बड़े कमरे में सोते हैं और चच्चो बेचारी अकेली पौर के पास के कमरे में ?
क्या ऐसा हो सकता है, मैंने सोचा, पौर के पास के दोनों कमरों को याद करके, जो दोनों रोशनदान से दीखते ही नहीं थे। एक तो लाइब्रेरी थी और दूसरा कबाड़खाना जहाँ दुनिया भर का टूटा, पुराना सामान, रद्दी में बिकने या नौकरों को देने-दिवाने तक जमा रहता। हिसाब की पुरानी डायरी स्कूल की भरी काँपियाँ टूटी आरामकुर्सी, जिसके नीचे अख़बार बिछाकर चाचा की बीमारी के शुरू के दिनों में उनके पलँग के पास कमोड ईजाद हुआ डब्बे, बोतलें, टीन के कनस्तर, बेकार कलम, पुराना फ्रिज जिसमें टाट की बोरियाँ ठुँसी थीं, पिंजरा, चूहेदानी कटा फटा होल्डौल और वह पीतल की पिचकारी जो होली पर नई-नई आई थी पर जितनी देखने में आलीशान थी उतनी ही रंग डालने में पिच्चकारी-पिच्च से एक महीन धार मारनेवाली-और जल्दी ही इसलिए कमरे में इक कोने में पड़कर होली की रौनक से अलग-थलग कर दी गई, और सुतली और खुर्पी और कानी पतीली और चूता बयाम। आँख मिचौली के दौरान मोहल्ले भर के बच्चों का जी होता उस कमरे में छिप जाएँ पर उस घर में पकड़े जाना ललना की डाँट और मां-बाप की गाहे-बगाहे चपत खाना था।
मैं उदास हो गया। न जाने कबाड़ याद करके ? या लाइब्रेरी में भरी किताबें ?
‘‘तो लाइब्रेरी थी ?’’ मेरी एक प्रेमिका ने बरसों बाद पूछा था शक़ निगाहों से छलक-छलक छलकाती।
‘‘हाँ।’’
‘‘तो गई कहाँ वह लाइब्रेरी ? उड़ गई ?’’
‘‘हां, उड़ गई।’’
‘‘वाह, पर लगे थे ?’’
‘‘हाँ पर लगे थे ।’’
‘‘रातोंरात फुर्र ?’’
मैं चुप हो गया। रातोंरात नहीं पर साल-दर-साल, धीरे-धीरे, चोरी-चोरी से। एक बार कोई कबाड़ी के पास से लाया-‘‘लीजिए’’-तीन किताबें, चाचा का नाम जिनमें था-‘‘लीजिए, अपनी समझिए !’’
‘‘तो, प्रेमिका ने सबूताना अन्दाज में कन्धे झटकाए, लाइब्रेरी वाइब्रेरी नहीं थी, वह कमरा था जहाँ चच्चो बेचारी अकेली सोती थी।’’
मैं गुमसुम था।
‘‘और ललना और चाचा साथ उधर।’’
‘‘अच्छा,’’ मैं शून्य स्वर में बोला।
‘‘बच्चों तक ने रोशनदान से देखा,’’ प्रेमिका ने झिड़का।
‘‘मैंने भी’’ मैंने उसे बताया।
‘‘तो कौन किसके संग सोता था ?’’
‘‘चाचा...’’
‘‘मेरे साथ।’’
‘‘उड़न-छू लाइब्रेरी में ?’’
‘‘नहीं, टट्टर के उधर बैठक में।’’
‘‘और बड़े कमरे में ?’’
‘‘चच्चो। ललना के साथ।’’
ललना।
जो उसका नाम नहीं।
उसका नाम किसी को नहीं पता।
कभी लोगों के रहस्य-भरे स्वरों से कुछ भान-मैंने पूछा, तो ललना जो मच्छरदानी के डंडे पर गीला पोंछा लपेटकर ऊपर चढ़ी पंखा साफ़ कर रही थी, इतने ज़ोर से हिली कि लगा कि गिरेगी और साथ मुझे और चच्चो को भी ले जाएगी और उस स्टूल को भी जिसे मेज़ पर चढ़ाकर हम दोनों कस के पकड़े थे और जिस पर खड़ी होकर ललना छत पर पहुँच गई थीं। ‘‘कौन कह रहा था कौन कह रहा था वही परेशवा होगा मना किया है न उसके संग मत घुसा रहा कर बहनजी आप तो कुछ कहती नहीं चौपट हो जाएगा लड़का हिलाओ नहीं’’ और बिगड़ी बात बनाने उसने डंडा पंखे पर न करके फ़र्श पर मारा कि गाड़ना हो हवा में घुमा के यों, कि पंखे की धूल नहीं, मेरी जिज्ञासा मेरे चेहरे से पोंछनी हो।
पर ललना उसका नाम नहीं।
क्या था किसी को नहीं पता। बस कहते कि आई थी रोती-बिसूरती कभी प्रेमानन्द जी के घर। तब मोहल्ला उसे लल्लन की बहू के नाम से जानने लगा।
पर वह लल्लन की बहू नहीं थी या जो आम समझा जाता है बहू के माने, उस माने से बहू नहीं थी। वह लल्लन की बहू नहीं, बीवी थी।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई नहीं जानता लल्लन कौन था ?’’ वही प्रेमिका, उन्हीं बरसों बाद के दिनों में, छत पर टंकी के पीछे आकर पूछने लगी। ‘‘यहाँ कोई न हो तो लोग पैदा कर लेते हैं, तुम कह रहे हो एक पूरा सलामत इंसान ग़ायब ?’’
छत की टंकी के पीछे मगर, शब्दों की गूँज दूसरी होती है। शब्द वही रहते हैं, मतलब बदलने लगते हैं। कोई नहीं जानता...हम तुम यहाँ...ग़ायब ग़ायब...सबकी नजरों से...ओ हो अय हय...!
‘‘सलामत कहाँ ?’’ मैंने दूसरी तरह की उतावली में प्रेमिका की गर्दन पर चढ़ाई-उतराई की।
‘‘पागल था ?’’
‘‘हाँ हाँ, पागल !’’ मैं हाँफा।
पर ये मुझे मालूम नहीं था। चच्चो ने कहा था कि ललना ने बताया। मर गया और लल्लन का बाप उसे धन्धे में बिठाना चाहता था इसलिए वह भाग आई।
‘‘भागकर कहाँ आई,’’ प्रेमिका बोली। ‘‘मैंने तो सुना है उसका ससुर उसे यहाँ लाया। खूब रोती-बिसूरती थी और ससुर के पाँव पकड़-पकड़ के कहती, ऐसा न करो बप्पा, छोड़ के मत ही जाइयो बप्पा, मर जाएगी तेरी बहुरिया बप्पा। कि रोने में उसकी नाक बहने लगी तो ससुर की ही धोती से वहीं उनके पैरों के पास वह नाक सुड़कती गई। हट-हट ससुर अपने पाँव उसके हाथ से नहीं, अपनी धोती उसकी नाक से बचा रहे थे।’’
अरे कहाँ की ले बैठी, मेरा मन टंकी के पीछे कुनमुनाया। ललना, चच्चो, चाचा ! करो मैं और तुम, अरे ! ये मौसम आशिकाना ! हम और तुम और ये समाँ ! रंगीं-रंगीं सी तनहाई ! इधर मैं जवाँ उधर तुम हँसीं !-ऐसे भाव मेरी हरकतों में।
‘‘क्या मालूम,’’ प्रेमिका की आँखें कल्पना के भ्रमण से उनींदी हो चलीं, ‘‘वह ससुर नहीं लल्लन ही था जो उसे छोड़ने आया कि इससे छुटकारा पा अपनी नई नवेली दूसरी दुलहिन के पास उड़ पहुंचे ?’’
‘‘हाँ...उसने...यह भी...ब...ताया था..।’’ मैंने अटक-अटक कर हामी भरी।
‘‘कि लल्लन ही था जो यहाँ आया ?’’ प्रेमिका की आँखें कोटरों के बाहर लपकीं।
‘‘नहीं, कि ललना उसकी दूसरी बीवी से तंग आकर भाग आई। ऐ बस।’’ मैंने तब कस के डाँटा।
कौन जाने वह कहाँ से आई ? सार यह कि आया था कोई कभी छोड़ने एक मिरगिल्ली रुअन्ती को, जिसके पैरों पर गिर वह नाक छिनकती रही, पर अन्तत: लोगों ने कहा कि ललना भागकर आ गई।
भागकर लल्लन से, जो कौन था कोई नहीं जानता, कहां का था, यह भी नहीं, था भी या नहीं किसी को दिलचस्पी नहीं, मानो सारी दिलचस्पी ललना ने चुम्बक लगाकर अपनी तरफ खींच ली हो।
लल्लन की बहू जिसे चाचा लल्लन की कहते और चच्चो ललना।
और मैं रंजिश से भर उठता हूँ कि जब हर तरफ चच्चो छाई हुई है तो यह क्यों आन धमकी है फिर से बीचोबीच ? चच्चो का कोई चिह्न हो जैसे। उसकी हर याद पर हावी।
कुछ भी अन्देशा नहीं था मुझे जब मैं घंटी सुनकर उठा !
बैठा था। चौंका भी नहीं। घंटी के स्वर पर एक नज़र टेलीफ़ोन पर डाली और उठकर सामने की तरफ जाने लगा।
दरवाजा खोला। नीचे पतंगों के परों का ढेर था जो हल्के से उड़ा और फिर वहीं जमा हो गया।
मैं खड़ा रहा, कुछ ऐसी प्रतीति में कि एक यही तो मैं करता रहा हूँ कब से दरवाज़ा खोला और ललना को सामने पाया। वह एक क्रिया, मात्र कुछ सेकेंड की, लकड़ी के दो पाटों को अलग-अलग तरफ सहज ढकेलना, मेरे जीवन में स्लो मोशन की निरन्तरता लिए जैसे होती ही रहती है। होती ही रहती है। स्लो मोशन में दरवाज़ा खोलता ही रहता हूँ। ललना उधर खड़ी मिलती ही रहती है।
मैं नीचे देखने लगा। ललना अन्दर आ गई। फिर मैं चुपचाप उसके पीछे घर में घुसता गया।
खाने की मेज पर घुचड़-मुचड़ पगड़िआई सी चद्दर को देखकर ललना ठिठक गई।
जम गया होगा, मैं बुदबुदाया था। पगड़ी खोली तो अन्दर कूँड़ी निकली। ग़ौर किया कि रात जब दूध रखा था तब हल्का था, अब जब दही उठा रहा हूं तो भारी हो चुका है।
ग़ौर नहीं किया कि अब मेरे दही जमाने के दिन गए।
किया होता तो शायद चच्चो की खिड़की पर चच्चो की कुर्सी खींचकर ललना को बैठने को न देता। ललना उसमें लुढ़क गयी और मैं खिड़की के बाहर नजर किये खड़ा हो गया। चुप।
जो ज़रा भी चुप नहीं था। धमकी-सा था कि आँधी बनकर भरता जाएगा और बाहर को फूट पड़ेगा।
अरे डेढ़ बज रहे हैं मैंने घड़ी देखी अभी तक जगी हो मैंने ललना को बताया मैं चच्चो से बोला।
चच्चो चुप रही बस आँखें घुमा के एक बार देखा मुझे मैंने बताया।
बहुत देर हो गयी अब सो जाओ मैंने बताया मैं बोला।
हाँ देर हो गयी अब सो जाऊँगी मैंने सपाट सुर में कहा चच्चो ने कहा तो ललना फूट-फूट कर रोने लगी कि जैसे चच्चो यह बता रही थी कि बस अब चिरनिद्रा में सो जाऊंगी।
मैं बत्ती बुझाकर चला गया मैंने कहा मानो कह रहा हूँ उसकी जीवन बत्ती ऑफ़ कर दी !
‘‘हाय मैं वहाँ होती तो,..’’ ललना बगल में आ खड़ी हुई मानो जो स्विच मैंने ऑफ़ किया वह फिर ऑन कर देती, होती तो।
चच्चो की मौत के पुनर्जन्म के उस पल में मगर, मैं इल्जाम की बातें भूल चुका था। बस यही है कि हम खड़े हैं चच्चो की याद में चच्चो की खिड़की पर। याद जिसमें से जीवन में घटी बातों का ब्यौरा धीरे-धीरे बह गया है और बस एक निराकार भास बन गया है।
मैंने तीली बुझाकर दूर बाहर उचकायी कि और है क्या याद करने को।
मेरी जली सिगरेट से ललना ने कश खींचे जैसे कुछ नहीं है भूलने को।
देर तक उस दिन वह चच्चो के कमरे में घूमती रही। कभी स्टूल पर चढ़कर रनर से निकल आए पर्दे के हुक वापस, अटकाती, कभी बरसात से फूल आए दरवाज़े को बार-बार पटक के बन्द करती, खोलती, फिर चच्चो की सारी किताबें शेल्फ़ से उतार, झटक-झटक कर ऊंचाई के हिसाब से कतार में खड़ी करती और कभी फिर खिड़की पर खड़ी !
वहीं जहाँ चच्चो खड़ी होती थी।
हाँ अब खा लूंगी बोली जब मैंने कहा देर हो रही है खा लो।
मुझे नहीं पता था कि यह मेरे कहे उससे आखिरी स्नेही शब्द हैं, कि एक बार फिर मैं उससे रूठकर कुट्टी करनेवाला हूँ।
मगर उसके मुझसे आखिरी शब्द नहीं थे जब वह बोली ‘‘चच्चो की गोदरेज की चाभी ?’’
थोड़ा मैंने तब देखा, ज़्यादा बाद में याद से देखता रहा कि बाकी दिन उसने चच्चो की एक-एक चीज़ निजी से निजी पहनने का कपड़ा महँगी से महँगी साड़ियाँ-सब निकालकर बिस्तर पर डाल दीं, पहले पूरी अलमारी गीले कपड़े से साफ़ की, सुखाई, हर खाने में ताज़ा, अख़बार बिछाया, फिर एक-एक कपड़ा एक-एक चीज़ खोली, झाड़ी, झटकी, पोंछी, तहाई, समेटी और अलमारी में नए सिरे से रखीं।
चच्चो की याद सँवारती या अपना भविष्य ?
ऑफिस से लौटकर अब मुझे घंटी बजानी पड़ती है।
बजाई थी। पहले दिन जब !
तब दरवाज़ा चरमरा के खुला और ललना उस तरफ खड़ी मिली। वह अन्दर मैं बाहर।
क्या मैं आँखें झिपझिपाते हुए उसे एकटक देखता रहा कि लो, कबसे होती आई वही क्रिया, बन्द दरवाज़े के दो पाट खुलने की, एक ओर वह, एक ओर मेरे होने की, फिर घटी ?
या उस दिन लगा कि इधर का पात्र उधर हो गया ?
हो सकता है मैं फौरन ही अन्दर चला गया, अपने मन में दरवाज़े के निरंतरता से खुलने को देखते-देखते। पौर से होते हुए ज़ीने के पास मेरे पाँव ठिठक गए। हो सकता है क्योंकि रसोईघर से जीरे और हींग की देशी घी में बघार की खुशबू उसी पल मुझ तक पहुँची। मानो पहला खटका तभी हुआ कि जिस हवा को इन दिनों मैंने घर-भर में बेहरकत ठहरने दिया था कि वह एक दोहर बनी मुझे लपेटे रहे, उसे बेधना शुरू हो गया है।
ये फिर आ गई है मुझे चच्चो की गोद से वंचित करने।
मैंने घबरा के दिशा बदली और सीधे ज़ीने के ऊपर चढ़ने लगा। दबे पाँव।
जैसे कभी चच्चो चढ़ती रही होगी।
ज़ीने के दरवाज़े पर उसके सीने में दिल करवटें लेने लगता। उसके पैरों में धुकधुकी होने लगती। दरवाज़े के पार पड़ी छत, छत नहीं, समन्दर-सी आ जा आ जा फुसफुसाती हो जैसे, जिस पुकार पर चच्चो खिंची तो चली आई है पर डर के भाग भी जाना चाह रही है।
छत नहीं, समुन्दर ही जैसे पूरे लेबरनम हाउस पर पड़ा था। पड़ा नहीं, डाटें मार रहा था। लम्बे-चौड़े लेबरनम हाउस पर, जो एक नहीं, कोई सौ सवा सौ घरों का पुराना मोहल्ला था, इस छोर से उस छोर दूर तक खिंची एक ही लम्बी-चौड़ी इमारत में बसा, कहीं ऊँची कहीं नीची लहरें भरती छत के नीचे, सदियों से डूबा पड़ा।
चाचा जान नहीं पाते। कि चुपचाप रहनेवाली, उनकी एक करारी नज़र पे सिमट जानेवाली चच्चो क्यों अचानक उठ बैठती है, क्या उसके मन में आता है जो पहले कि वह उसे पकड़ पाए पंख बनकर ऊपर उड़ जाता है, ताकि वह और बेचैन हो जाए, ज़ीने पर अनायास चढ़ने लगे मानो किसी ने उसे कोहनी गडोई है-उट्ठो नींद नहीं आ रही हाँ नहीं आ रही मुझे भी तो चलो न चलें छत पर।
ज़ीने का दरवाज़ा खोलकर चच्चो खड़ी है।
बरसात के बचे-खुचे दिन। दूर-दूर तक फैली छत। उसका भीगा-भीगा सुरमई सम्मोहन। उसका धीरे-धीरे लहराना। उसका लहरा-लहरा के सुरमई बाँहें उठाना। बाँहें उठाकर आकाश को तारों समेत हल्के-हल्के खींचना। आँखों में उनकी टिमटिमाहट का तैर जाना।
जब पैरों के नीचे छत हो तो ऊपर पूरा आकाश है।
हम चलने लगे हैं-चच्चो की याद और मैं।
अभी चच्चो की बाँहों के अन्दर मांस ने पानी बनना नहीं शुरू किया है इसलिए हम सबकी नज़रों से बचकर चलेंगे, अँधेरे में राह बनाते। चच्चो अपनी गोल सख़्त बाँह से खुद ही टकराकर हल्के से सहम गई है !
जहाँ-तहाँ छत का लेवल बदलेगा, दो-तीन सीढ़ी चढ़नी या उतरनी पड़ेगी। या फिर टंकी पर चढ़कर कूद जाओ। या छज्जे से लपक लो। तो फिर चच्चो को अपनी साड़ी टखनों से ऊपर समेटनी पड़ेगी।
पड़ी।
उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। दूर किनारे पर नौकरों ने अपने मालिकों की खाटें लगा दी हैं। अँधेरे की उजाली छायाएँ।
हल्की सी हवा चच्चो की साड़ी को उड़ाती है तो चच्चो घुटनों तक उसे उठा लेती है और सफ़ाई से मुँडेर पर चढ़, जैसे तनी रस्सी पर चलती हुई उधर कूद जाती है।
वह भी, मैं भी।
इसी छत की बात है-कि मोहल्ले के बच्चे एक दूसरे की नकल-नकलाई में पड़ और बालिगों की कही-सुनाई पे उछल इक्कड़-दुक्कड़ खेलते-खेलते नाहक बीच में टाइम्स चिल्ला देते और दौड़ जाते इस घर के रोशनदान से नीचे झाँकने और नर्वस सी खिलखिलाई शुरू करने। मैं खुद उनके साथ दौड़ जाता और कमरे में झाँकने लगता और मुझसे बड़े बच्चे पकड़ते मेरी निकर और धमकाते-
बोल देखा न जो हमने देखा,
ढन ढन ढन ढन होते देखा !
तो मैं कसके निकर को ऊपर खींचे रखता और उन्हें खुश करने को चिल्लाता-
देखा मैंने ढन ढन देखा।
ढन ढन पर सिर मज़े से डुलाता जिस पर सबके साथ मैं भी हँस देता और वापस गुट्टी फेंककर एक पैर पर कूदने लगता।
बड़े लेकिन, झाँकने के बाद, इक्कड़-दुक्कड़ नहीं खेलते। रोशनदान का एन्शेन्ट धूमिल-धूसरित चटका शीशा वह जादू के चश्मे का शीशा था जिसके पार से आकर कहानियाँ हिंडोला बन जातीं और इस छत पर ढेंरों पूरे वयस्क लोग बस झूलते जाते, मचल-मचल जाते, मोहल्ले भर की हवा में ऊँची-ऊँची पेंगों की फूँक भर देते।
देख लिया न, वह पूछते। बच्चों ने भी तो यही देखा, बच्चे तो झूठ नहीं बोलते, बच्चे तो मन के सच्चे हैं न, नहीं, वह अपने विश्वास की दीवार बनाते। रोशनदान से नीचे झाँका तो यही न देखा कि चाचा और ललना बड़े कमरे में सोते हैं और चच्चो बेचारी अकेली पौर के पास के कमरे में ?
क्या ऐसा हो सकता है, मैंने सोचा, पौर के पास के दोनों कमरों को याद करके, जो दोनों रोशनदान से दीखते ही नहीं थे। एक तो लाइब्रेरी थी और दूसरा कबाड़खाना जहाँ दुनिया भर का टूटा, पुराना सामान, रद्दी में बिकने या नौकरों को देने-दिवाने तक जमा रहता। हिसाब की पुरानी डायरी स्कूल की भरी काँपियाँ टूटी आरामकुर्सी, जिसके नीचे अख़बार बिछाकर चाचा की बीमारी के शुरू के दिनों में उनके पलँग के पास कमोड ईजाद हुआ डब्बे, बोतलें, टीन के कनस्तर, बेकार कलम, पुराना फ्रिज जिसमें टाट की बोरियाँ ठुँसी थीं, पिंजरा, चूहेदानी कटा फटा होल्डौल और वह पीतल की पिचकारी जो होली पर नई-नई आई थी पर जितनी देखने में आलीशान थी उतनी ही रंग डालने में पिच्चकारी-पिच्च से एक महीन धार मारनेवाली-और जल्दी ही इसलिए कमरे में इक कोने में पड़कर होली की रौनक से अलग-थलग कर दी गई, और सुतली और खुर्पी और कानी पतीली और चूता बयाम। आँख मिचौली के दौरान मोहल्ले भर के बच्चों का जी होता उस कमरे में छिप जाएँ पर उस घर में पकड़े जाना ललना की डाँट और मां-बाप की गाहे-बगाहे चपत खाना था।
मैं उदास हो गया। न जाने कबाड़ याद करके ? या लाइब्रेरी में भरी किताबें ?
‘‘तो लाइब्रेरी थी ?’’ मेरी एक प्रेमिका ने बरसों बाद पूछा था शक़ निगाहों से छलक-छलक छलकाती।
‘‘हाँ।’’
‘‘तो गई कहाँ वह लाइब्रेरी ? उड़ गई ?’’
‘‘हां, उड़ गई।’’
‘‘वाह, पर लगे थे ?’’
‘‘हाँ पर लगे थे ।’’
‘‘रातोंरात फुर्र ?’’
मैं चुप हो गया। रातोंरात नहीं पर साल-दर-साल, धीरे-धीरे, चोरी-चोरी से। एक बार कोई कबाड़ी के पास से लाया-‘‘लीजिए’’-तीन किताबें, चाचा का नाम जिनमें था-‘‘लीजिए, अपनी समझिए !’’
‘‘तो, प्रेमिका ने सबूताना अन्दाज में कन्धे झटकाए, लाइब्रेरी वाइब्रेरी नहीं थी, वह कमरा था जहाँ चच्चो बेचारी अकेली सोती थी।’’
मैं गुमसुम था।
‘‘और ललना और चाचा साथ उधर।’’
‘‘अच्छा,’’ मैं शून्य स्वर में बोला।
‘‘बच्चों तक ने रोशनदान से देखा,’’ प्रेमिका ने झिड़का।
‘‘मैंने भी’’ मैंने उसे बताया।
‘‘तो कौन किसके संग सोता था ?’’
‘‘चाचा...’’
‘‘मेरे साथ।’’
‘‘उड़न-छू लाइब्रेरी में ?’’
‘‘नहीं, टट्टर के उधर बैठक में।’’
‘‘और बड़े कमरे में ?’’
‘‘चच्चो। ललना के साथ।’’
ललना।
जो उसका नाम नहीं।
उसका नाम किसी को नहीं पता।
कभी लोगों के रहस्य-भरे स्वरों से कुछ भान-मैंने पूछा, तो ललना जो मच्छरदानी के डंडे पर गीला पोंछा लपेटकर ऊपर चढ़ी पंखा साफ़ कर रही थी, इतने ज़ोर से हिली कि लगा कि गिरेगी और साथ मुझे और चच्चो को भी ले जाएगी और उस स्टूल को भी जिसे मेज़ पर चढ़ाकर हम दोनों कस के पकड़े थे और जिस पर खड़ी होकर ललना छत पर पहुँच गई थीं। ‘‘कौन कह रहा था कौन कह रहा था वही परेशवा होगा मना किया है न उसके संग मत घुसा रहा कर बहनजी आप तो कुछ कहती नहीं चौपट हो जाएगा लड़का हिलाओ नहीं’’ और बिगड़ी बात बनाने उसने डंडा पंखे पर न करके फ़र्श पर मारा कि गाड़ना हो हवा में घुमा के यों, कि पंखे की धूल नहीं, मेरी जिज्ञासा मेरे चेहरे से पोंछनी हो।
पर ललना उसका नाम नहीं।
क्या था किसी को नहीं पता। बस कहते कि आई थी रोती-बिसूरती कभी प्रेमानन्द जी के घर। तब मोहल्ला उसे लल्लन की बहू के नाम से जानने लगा।
पर वह लल्लन की बहू नहीं थी या जो आम समझा जाता है बहू के माने, उस माने से बहू नहीं थी। वह लल्लन की बहू नहीं, बीवी थी।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई नहीं जानता लल्लन कौन था ?’’ वही प्रेमिका, उन्हीं बरसों बाद के दिनों में, छत पर टंकी के पीछे आकर पूछने लगी। ‘‘यहाँ कोई न हो तो लोग पैदा कर लेते हैं, तुम कह रहे हो एक पूरा सलामत इंसान ग़ायब ?’’
छत की टंकी के पीछे मगर, शब्दों की गूँज दूसरी होती है। शब्द वही रहते हैं, मतलब बदलने लगते हैं। कोई नहीं जानता...हम तुम यहाँ...ग़ायब ग़ायब...सबकी नजरों से...ओ हो अय हय...!
‘‘सलामत कहाँ ?’’ मैंने दूसरी तरह की उतावली में प्रेमिका की गर्दन पर चढ़ाई-उतराई की।
‘‘पागल था ?’’
‘‘हाँ हाँ, पागल !’’ मैं हाँफा।
पर ये मुझे मालूम नहीं था। चच्चो ने कहा था कि ललना ने बताया। मर गया और लल्लन का बाप उसे धन्धे में बिठाना चाहता था इसलिए वह भाग आई।
‘‘भागकर कहाँ आई,’’ प्रेमिका बोली। ‘‘मैंने तो सुना है उसका ससुर उसे यहाँ लाया। खूब रोती-बिसूरती थी और ससुर के पाँव पकड़-पकड़ के कहती, ऐसा न करो बप्पा, छोड़ के मत ही जाइयो बप्पा, मर जाएगी तेरी बहुरिया बप्पा। कि रोने में उसकी नाक बहने लगी तो ससुर की ही धोती से वहीं उनके पैरों के पास वह नाक सुड़कती गई। हट-हट ससुर अपने पाँव उसके हाथ से नहीं, अपनी धोती उसकी नाक से बचा रहे थे।’’
अरे कहाँ की ले बैठी, मेरा मन टंकी के पीछे कुनमुनाया। ललना, चच्चो, चाचा ! करो मैं और तुम, अरे ! ये मौसम आशिकाना ! हम और तुम और ये समाँ ! रंगीं-रंगीं सी तनहाई ! इधर मैं जवाँ उधर तुम हँसीं !-ऐसे भाव मेरी हरकतों में।
‘‘क्या मालूम,’’ प्रेमिका की आँखें कल्पना के भ्रमण से उनींदी हो चलीं, ‘‘वह ससुर नहीं लल्लन ही था जो उसे छोड़ने आया कि इससे छुटकारा पा अपनी नई नवेली दूसरी दुलहिन के पास उड़ पहुंचे ?’’
‘‘हाँ...उसने...यह भी...ब...ताया था..।’’ मैंने अटक-अटक कर हामी भरी।
‘‘कि लल्लन ही था जो यहाँ आया ?’’ प्रेमिका की आँखें कोटरों के बाहर लपकीं।
‘‘नहीं, कि ललना उसकी दूसरी बीवी से तंग आकर भाग आई। ऐ बस।’’ मैंने तब कस के डाँटा।
कौन जाने वह कहाँ से आई ? सार यह कि आया था कोई कभी छोड़ने एक मिरगिल्ली रुअन्ती को, जिसके पैरों पर गिर वह नाक छिनकती रही, पर अन्तत: लोगों ने कहा कि ललना भागकर आ गई।
भागकर लल्लन से, जो कौन था कोई नहीं जानता, कहां का था, यह भी नहीं, था भी या नहीं किसी को दिलचस्पी नहीं, मानो सारी दिलचस्पी ललना ने चुम्बक लगाकर अपनी तरफ खींच ली हो।
लल्लन की बहू जिसे चाचा लल्लन की कहते और चच्चो ललना।
और मैं रंजिश से भर उठता हूँ कि जब हर तरफ चच्चो छाई हुई है तो यह क्यों आन धमकी है फिर से बीचोबीच ? चच्चो का कोई चिह्न हो जैसे। उसकी हर याद पर हावी।
कुछ भी अन्देशा नहीं था मुझे जब मैं घंटी सुनकर उठा !
बैठा था। चौंका भी नहीं। घंटी के स्वर पर एक नज़र टेलीफ़ोन पर डाली और उठकर सामने की तरफ जाने लगा।
दरवाजा खोला। नीचे पतंगों के परों का ढेर था जो हल्के से उड़ा और फिर वहीं जमा हो गया।
मैं खड़ा रहा, कुछ ऐसी प्रतीति में कि एक यही तो मैं करता रहा हूँ कब से दरवाज़ा खोला और ललना को सामने पाया। वह एक क्रिया, मात्र कुछ सेकेंड की, लकड़ी के दो पाटों को अलग-अलग तरफ सहज ढकेलना, मेरे जीवन में स्लो मोशन की निरन्तरता लिए जैसे होती ही रहती है। होती ही रहती है। स्लो मोशन में दरवाज़ा खोलता ही रहता हूँ। ललना उधर खड़ी मिलती ही रहती है।
मैं नीचे देखने लगा। ललना अन्दर आ गई। फिर मैं चुपचाप उसके पीछे घर में घुसता गया।
खाने की मेज पर घुचड़-मुचड़ पगड़िआई सी चद्दर को देखकर ललना ठिठक गई।
जम गया होगा, मैं बुदबुदाया था। पगड़ी खोली तो अन्दर कूँड़ी निकली। ग़ौर किया कि रात जब दूध रखा था तब हल्का था, अब जब दही उठा रहा हूं तो भारी हो चुका है।
ग़ौर नहीं किया कि अब मेरे दही जमाने के दिन गए।
किया होता तो शायद चच्चो की खिड़की पर चच्चो की कुर्सी खींचकर ललना को बैठने को न देता। ललना उसमें लुढ़क गयी और मैं खिड़की के बाहर नजर किये खड़ा हो गया। चुप।
जो ज़रा भी चुप नहीं था। धमकी-सा था कि आँधी बनकर भरता जाएगा और बाहर को फूट पड़ेगा।
अरे डेढ़ बज रहे हैं मैंने घड़ी देखी अभी तक जगी हो मैंने ललना को बताया मैं चच्चो से बोला।
चच्चो चुप रही बस आँखें घुमा के एक बार देखा मुझे मैंने बताया।
बहुत देर हो गयी अब सो जाओ मैंने बताया मैं बोला।
हाँ देर हो गयी अब सो जाऊँगी मैंने सपाट सुर में कहा चच्चो ने कहा तो ललना फूट-फूट कर रोने लगी कि जैसे चच्चो यह बता रही थी कि बस अब चिरनिद्रा में सो जाऊंगी।
मैं बत्ती बुझाकर चला गया मैंने कहा मानो कह रहा हूँ उसकी जीवन बत्ती ऑफ़ कर दी !
‘‘हाय मैं वहाँ होती तो,..’’ ललना बगल में आ खड़ी हुई मानो जो स्विच मैंने ऑफ़ किया वह फिर ऑन कर देती, होती तो।
चच्चो की मौत के पुनर्जन्म के उस पल में मगर, मैं इल्जाम की बातें भूल चुका था। बस यही है कि हम खड़े हैं चच्चो की याद में चच्चो की खिड़की पर। याद जिसमें से जीवन में घटी बातों का ब्यौरा धीरे-धीरे बह गया है और बस एक निराकार भास बन गया है।
मैंने तीली बुझाकर दूर बाहर उचकायी कि और है क्या याद करने को।
मेरी जली सिगरेट से ललना ने कश खींचे जैसे कुछ नहीं है भूलने को।
देर तक उस दिन वह चच्चो के कमरे में घूमती रही। कभी स्टूल पर चढ़कर रनर से निकल आए पर्दे के हुक वापस, अटकाती, कभी बरसात से फूल आए दरवाज़े को बार-बार पटक के बन्द करती, खोलती, फिर चच्चो की सारी किताबें शेल्फ़ से उतार, झटक-झटक कर ऊंचाई के हिसाब से कतार में खड़ी करती और कभी फिर खिड़की पर खड़ी !
वहीं जहाँ चच्चो खड़ी होती थी।
हाँ अब खा लूंगी बोली जब मैंने कहा देर हो रही है खा लो।
मुझे नहीं पता था कि यह मेरे कहे उससे आखिरी स्नेही शब्द हैं, कि एक बार फिर मैं उससे रूठकर कुट्टी करनेवाला हूँ।
मगर उसके मुझसे आखिरी शब्द नहीं थे जब वह बोली ‘‘चच्चो की गोदरेज की चाभी ?’’
थोड़ा मैंने तब देखा, ज़्यादा बाद में याद से देखता रहा कि बाकी दिन उसने चच्चो की एक-एक चीज़ निजी से निजी पहनने का कपड़ा महँगी से महँगी साड़ियाँ-सब निकालकर बिस्तर पर डाल दीं, पहले पूरी अलमारी गीले कपड़े से साफ़ की, सुखाई, हर खाने में ताज़ा, अख़बार बिछाया, फिर एक-एक कपड़ा एक-एक चीज़ खोली, झाड़ी, झटकी, पोंछी, तहाई, समेटी और अलमारी में नए सिरे से रखीं।
चच्चो की याद सँवारती या अपना भविष्य ?
ऑफिस से लौटकर अब मुझे घंटी बजानी पड़ती है।
बजाई थी। पहले दिन जब !
तब दरवाज़ा चरमरा के खुला और ललना उस तरफ खड़ी मिली। वह अन्दर मैं बाहर।
क्या मैं आँखें झिपझिपाते हुए उसे एकटक देखता रहा कि लो, कबसे होती आई वही क्रिया, बन्द दरवाज़े के दो पाट खुलने की, एक ओर वह, एक ओर मेरे होने की, फिर घटी ?
या उस दिन लगा कि इधर का पात्र उधर हो गया ?
हो सकता है मैं फौरन ही अन्दर चला गया, अपने मन में दरवाज़े के निरंतरता से खुलने को देखते-देखते। पौर से होते हुए ज़ीने के पास मेरे पाँव ठिठक गए। हो सकता है क्योंकि रसोईघर से जीरे और हींग की देशी घी में बघार की खुशबू उसी पल मुझ तक पहुँची। मानो पहला खटका तभी हुआ कि जिस हवा को इन दिनों मैंने घर-भर में बेहरकत ठहरने दिया था कि वह एक दोहर बनी मुझे लपेटे रहे, उसे बेधना शुरू हो गया है।
ये फिर आ गई है मुझे चच्चो की गोद से वंचित करने।
मैंने घबरा के दिशा बदली और सीधे ज़ीने के ऊपर चढ़ने लगा। दबे पाँव।
जैसे कभी चच्चो चढ़ती रही होगी।
ज़ीने के दरवाज़े पर उसके सीने में दिल करवटें लेने लगता। उसके पैरों में धुकधुकी होने लगती। दरवाज़े के पार पड़ी छत, छत नहीं, समन्दर-सी आ जा आ जा फुसफुसाती हो जैसे, जिस पुकार पर चच्चो खिंची तो चली आई है पर डर के भाग भी जाना चाह रही है।
छत नहीं, समुन्दर ही जैसे पूरे लेबरनम हाउस पर पड़ा था। पड़ा नहीं, डाटें मार रहा था। लम्बे-चौड़े लेबरनम हाउस पर, जो एक नहीं, कोई सौ सवा सौ घरों का पुराना मोहल्ला था, इस छोर से उस छोर दूर तक खिंची एक ही लम्बी-चौड़ी इमारत में बसा, कहीं ऊँची कहीं नीची लहरें भरती छत के नीचे, सदियों से डूबा पड़ा।
चाचा जान नहीं पाते। कि चुपचाप रहनेवाली, उनकी एक करारी नज़र पे सिमट जानेवाली चच्चो क्यों अचानक उठ बैठती है, क्या उसके मन में आता है जो पहले कि वह उसे पकड़ पाए पंख बनकर ऊपर उड़ जाता है, ताकि वह और बेचैन हो जाए, ज़ीने पर अनायास चढ़ने लगे मानो किसी ने उसे कोहनी गडोई है-उट्ठो नींद नहीं आ रही हाँ नहीं आ रही मुझे भी तो चलो न चलें छत पर।
ज़ीने का दरवाज़ा खोलकर चच्चो खड़ी है।
बरसात के बचे-खुचे दिन। दूर-दूर तक फैली छत। उसका भीगा-भीगा सुरमई सम्मोहन। उसका धीरे-धीरे लहराना। उसका लहरा-लहरा के सुरमई बाँहें उठाना। बाँहें उठाकर आकाश को तारों समेत हल्के-हल्के खींचना। आँखों में उनकी टिमटिमाहट का तैर जाना।
जब पैरों के नीचे छत हो तो ऊपर पूरा आकाश है।
हम चलने लगे हैं-चच्चो की याद और मैं।
अभी चच्चो की बाँहों के अन्दर मांस ने पानी बनना नहीं शुरू किया है इसलिए हम सबकी नज़रों से बचकर चलेंगे, अँधेरे में राह बनाते। चच्चो अपनी गोल सख़्त बाँह से खुद ही टकराकर हल्के से सहम गई है !
जहाँ-तहाँ छत का लेवल बदलेगा, दो-तीन सीढ़ी चढ़नी या उतरनी पड़ेगी। या फिर टंकी पर चढ़कर कूद जाओ। या छज्जे से लपक लो। तो फिर चच्चो को अपनी साड़ी टखनों से ऊपर समेटनी पड़ेगी।
पड़ी।
उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। दूर किनारे पर नौकरों ने अपने मालिकों की खाटें लगा दी हैं। अँधेरे की उजाली छायाएँ।
हल्की सी हवा चच्चो की साड़ी को उड़ाती है तो चच्चो घुटनों तक उसे उठा लेती है और सफ़ाई से मुँडेर पर चढ़, जैसे तनी रस्सी पर चलती हुई उधर कूद जाती है।
वह भी, मैं भी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i