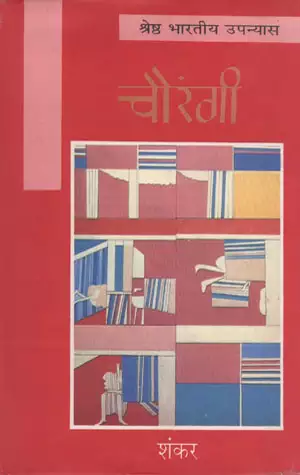|
सामाजिक >> चौरंगी चौरंगीशंकर
|
363 पाठक हैं |
|||||||
सुखी और दुखी, सहयोगी और विरोधी, उत्कर्ष और पतन, आदर्श और व्यवहार, व्यावसायिक और मानवीय-बहुनिधि मानव चरित्रों की कथा है यह उपन्यास
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
सुखी और दुखी, सहयोगी और विरोधी, उत्कर्ष और पतन, आदर्श और व्यवहार,
व्यावसायिक और मानवीय-बहुनिधि मानव चरित्रों की कथा है यह उपन्यास,
चौरंगी। शाहजहाँ होटल के माध्यम से लेखक केवल कलकत्ता का चित्र नहीं बल्कि
सम्पूर्ण मानव व्यवहार का चित्र प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास में इतने
अधिक विविधिरंगी चरित्र हैं कि इसे सहज ही मानव जीवन की महागाथा कहा जा
सकता है पर महागाथाओं की तरह इसमें कोई महानायक नहीं है इसलिए यह उपन्यास
कोई आदर्श भी नहीं रचता। यह केवल परत-दर-परत मानवीय व्यवहार के विभिन्न
पहलुओं को खोलता रहता है। यही वजह है कि कई बार एक ही व्यक्ति के चरित्र
के दो रूप उभर कर सामने आते हैं।
महानगरीय जीवन की महत्वाकाक्षांओं के बीच किस तरह से इच्छाएँ और सम्बन्ध दम तोड़ जाते हैं यह इसमें बाखूबी देखा जा सकता है। परन्तु कभी भी सब कुछ नष्ट नहीं होता। नष्ट होने के बीच बहुत कुछ ऐसा बचा रहता है जो नये निर्माण की आशा को जीवित रखता है। बहुरंगी चरित्रों की इस महागाथा को बाँधे रखने वाला एकमात्र सूत्र है, सहज मानवीय स्नेह। शाहजहाँ होटल में काम करते हुए नायक को सबसे अधिक ऐश्वर्य जो मिला वह था साथ काम करने वालों का स्नेह। और यही स्नेह सबकुछ नष्ट हो जाने के बीच भी निर्माण की आशा को बरकरार रखता है।
सृष्टि में जितना आनंद था, जितना सौंदर्य था, सारा कुछ पृथ्वी के अविचारी मनुष्यों ने समाप्त कर दिया है। बच गया है केवल दुख। किसी के लिए भी, कहीं भी सुख का एक कण नहीं है !
लिख-पढ़कर इस अन्धी-गूँगी व्यावसायिक सभ्यता को बदला नहीं जा सकता, हिलाया तक नहीं जा सकता।....माइक पर चीखो-चिल्लाओ, महाभारत जैसी दस पौण्ड वजन की किताब लिख मारो, हज़ार-हज़ार पावर की बत्ती से इस सभ्यता के जख्मों पर रोशनी डालो, फिर भी कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा !
हे परमपिता, तुम्हारा अभिशाप इस ऐश्वर्य और साथ ही कुत्सित, वीभत्स सभ्यता पर वज्र बनकर गिरे !
‘चौरंगी लिखने की प्रथम अनुप्रेरणा जिनसे मिली थी, वह श्रद्धेय विदेशी महापुरुष अब परलोकवासी हैं। जीवित एवं मृत, देशी एवं विदेशी, परिचित एवं अपरिचित, जिन व्यक्तियों ने प्रकट तथा परोक्ष रूप से यह पुस्तक लिखने में विभिन्न प्रकार की सहायता मुझे की है, उन सभी के प्रति मेरा सश्रद्ध नमस्कार निवेदित है।
महानगरीय जीवन की महत्वाकाक्षांओं के बीच किस तरह से इच्छाएँ और सम्बन्ध दम तोड़ जाते हैं यह इसमें बाखूबी देखा जा सकता है। परन्तु कभी भी सब कुछ नष्ट नहीं होता। नष्ट होने के बीच बहुत कुछ ऐसा बचा रहता है जो नये निर्माण की आशा को जीवित रखता है। बहुरंगी चरित्रों की इस महागाथा को बाँधे रखने वाला एकमात्र सूत्र है, सहज मानवीय स्नेह। शाहजहाँ होटल में काम करते हुए नायक को सबसे अधिक ऐश्वर्य जो मिला वह था साथ काम करने वालों का स्नेह। और यही स्नेह सबकुछ नष्ट हो जाने के बीच भी निर्माण की आशा को बरकरार रखता है।
सृष्टि में जितना आनंद था, जितना सौंदर्य था, सारा कुछ पृथ्वी के अविचारी मनुष्यों ने समाप्त कर दिया है। बच गया है केवल दुख। किसी के लिए भी, कहीं भी सुख का एक कण नहीं है !
लिख-पढ़कर इस अन्धी-गूँगी व्यावसायिक सभ्यता को बदला नहीं जा सकता, हिलाया तक नहीं जा सकता।....माइक पर चीखो-चिल्लाओ, महाभारत जैसी दस पौण्ड वजन की किताब लिख मारो, हज़ार-हज़ार पावर की बत्ती से इस सभ्यता के जख्मों पर रोशनी डालो, फिर भी कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा !
हे परमपिता, तुम्हारा अभिशाप इस ऐश्वर्य और साथ ही कुत्सित, वीभत्स सभ्यता पर वज्र बनकर गिरे !
‘चौरंगी लिखने की प्रथम अनुप्रेरणा जिनसे मिली थी, वह श्रद्धेय विदेशी महापुरुष अब परलोकवासी हैं। जीवित एवं मृत, देशी एवं विदेशी, परिचित एवं अपरिचित, जिन व्यक्तियों ने प्रकट तथा परोक्ष रूप से यह पुस्तक लिखने में विभिन्न प्रकार की सहायता मुझे की है, उन सभी के प्रति मेरा सश्रद्ध नमस्कार निवेदित है।
-शंकर
Our life is but a winter’s day :
Some only breakfast and away,
Others to dinner stay and are full fed ;
The oldest man but sups and goes to bed ;
He that goes soonest has the least to pay.
Some only breakfast and away,
Others to dinner stay and are full fed ;
The oldest man but sups and goes to bed ;
He that goes soonest has the least to pay.
-A.C. Maffen.
एक
वे लोग कहते हैं—एस्प्लेनेड। हम लोग कहते हैं—चौरंगी।
इस
चौरंगी का कर्जन पार्क। सारा दिन घूमते रहने के कारण थका हुआ शरीर जब एक
कदम भी चलने से इन्कार करने लगा, तब इसी पार्क में आश्रय मिला। महामान्य
इतिहास-पुरुष कर्ज़न साहब एक युग पहले बंगाल के लिए अभिशाप बनकर आये थे।
सुजला-सुफला इस धरती को दो हिस्सों में बाँट देने की कुबुद्धि जब उनके मन
में उपजी थी, कहते हैं, हम लोगों के दुर्दिन का इतिहास उसी दिन से शुरू
हुआ था। मगर, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। बीसवीं शताब्दी की इस भरी
दोपहरी में, मई महीने की धूप से जलते हुए इस कलकत्ता महानगर की छाती पर
खड़े होकर मैंने इतिहास के पन्नों पर बार-बार धिक्कारे गये उस प्रतिभावान
अंग्रेज़ राजपुरुष को मन-ही-मन प्रणाम किया, उसकी स्वर्गीय आत्मा की
सद्गति के लिए मैंने प्रार्थना की, और प्रणाम किया मैंने राय हरिराम
गोयन्का बहादुर के.सी.आई.ई. को (कर्ज़न पार्क में जिनकी संगमरमरी मूर्ति
प्रतिष्ठित है), जिनके पाँवों के नीचे की पीठिका पर लिखा
है—जन्म :
जून 3, 1862 ;मृत्यु : फ़रवरी 28, 1935।
क्या मैं आप लोगों को अब तक याद हूँ ? बहुत दिनों पहले का सुन्दर एक अपरिपक्व-बुद्धि बालक अपने विभूति भाई का हाथ पकड़कर रामकृष्णपुर घाट से ‘अम्बा’ स्टीमर पर गंगा पार करके कलकत्ता हाईकोर्ट देखने आया था। 1अंग्रेज़ बैरिस्टर साहब के पास उसे नौकरी मिल गयी थी। उनका प्यार भी मिला था। जज, बैरिस्टर मुवक्किल—सबका स्नेह सत्कार पाकर वह प्राणपण से किरानीगिरी कर सका था, और चकित आँखों से, विस्मित दृष्टि से इस अपरिचित-अनजान दुनिया के रूप, रस, गन्धों का उपभोग कर सका था।
दुःख और दरिद्रता की अन्तहीन मरुभूमि में अचानक संसार-प्रेमी विदेशी बैरिस्टर के उपवन का आश्रय पाकर मेरी भूखी और थकी हुई आत्मा अपने सारे अतीत को भूल गई थी। मैं सोचने लगा था,
-----------------------------------------------------
1लेखक के उपन्यास ‘कितने अनजान रे’ का आरम्भिक प्रसंग।
शायद यह आश्रय कभी टूटेगा नहीं, चिरकाल तक स्थायी रहेगा। लेकिन लगता है, विधाता के सतर्क, चतुर ऑडीटरों की जमात हिसाब-किताब की गलतियाँ पकड़ने के लिए हमेशा घूमती-भागती रहती है। मेरे हिसाब की गलती पकड़ने में भी उन्हें जरा-सी देर न हुई। बैरिस्टर साहब का देहान्त हो गया, और मरुभूमि का वह ‘ओसिस’ जलकर राख हो गया। मरुभूमि में गढ़ा हुआ हमारा तम्बू रेगिस्तानी हवा के एक ही झोंके से उड़ गया। पता नहीं, कहाँ चला गया। ‘फिर से चलना शुरू करो ! फॉरवर्ड मार्च !’ विजय विधाता के हृदयहीन सेनापति ने इस हारे हुए कैदी को आज्ञा दी। आत्मा गवाही नहीं देती थी, फिर भी तरह-तरह के आघातों से क्षत-विक्षत हो गये अपने मन को, अपने थके हुए, टूटे हुए शरीर की रेलगाड़ी पर चढ़ाकर आगे बढ़ाना ही पड़ा। यात्रा शुरू करनी ही पड़ी। ‘आगे बढ़ो ! पीछे की ओर मत देखो !’
मेरे सामने सूनसान रास्ता है, और मेरे पीछे सूनसान रास्ता है। लगता है, रात के अँधेरे में मैं ओल्ड पोस्ट ऑफ़िस स्ट्रीट की अनजानी और पुरानी सराय में टिक गया था। अब सुबह की रोशनी में फिर सड़क पर उतर आया हूँ। हाईकोर्ट के बाबू लोग मुझे देखने आये थे। सहानुभूति दरसा गये थे। छोका भाई ने कहा था, ‘‘उफ़, इसी उम्र में अपना मालिक खो बैठे हो, अपना घर तोड़ बैठे हो ! इतनी कच्ची उम्र में !’’
लेकिन, मैं रोया नहीं था। एक बूँद भी आँसू मेरी आँखों से नहीं टपका। इस वज्राघात से जैसे मेरी आँखों का सारा पानी धुआँ बनकर उड़ गया था।
छोका भाई ने पास बुलाकर बिठाया था। सरदारजी की दुकान से चाय मँगा ली थी। बोले थे, ‘‘समझता हूँ भाई, सब समझता हूँ। मगर, यह पापी पेट कुछ करने नहीं देता, कुछ समझने नहीं देता। देखो, जो कुछ भी मिले, उसे ग्रहण करो। पेट भरते रहो, तभी जीवित रह सकोगे। शरीर को बल मिलेगा।’’
ओल्ड पोस्ट ऑफ़िस स्ट्रीट में मैं आखिरी बार चाय पी रहा था। फिर कभी उधर जा ही नहीं पाया। यों छोका भाई ने कहा जरूर था, ‘‘चिन्ता मत करो। इसी इलाके में तुम्हारा कुछ-न-कुछ इन्तज़ाम हो जायेगा। कौन साहब ऐसा है, जो तुम्हारे जैसे किरानी को नौकरी देना नहीं चाहेगा ! हाँ, यह बात जरूर है कि एक बीवी के रहते दूसरी बीवी बुला लेना...! हर साहब के पास कोई-न-कोई किरानी तो है ही।’’
किसी बात पर जोर देना, किसी पर दबाव डालना मेरे स्वभाव के विपरीत है। मगर, उस दिन मैं चुप नहीं रह सका था। पूरी ताक़त से मैंने कहा था, ‘‘छोका भाई, मुझसे नहीं होगा। नौकरी मिल भी जाये, मगर, अब इस मुहल्ले में रहना मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगा।’’
छोका भाई, अर्जुन भाई, हारू भाई, उस दिन सभी व्यक्ति मेरे दुःख से अभीभूत हो गये थे। विषण्ण होकर छोका भाई ने कहा था, ‘‘हम लोग तो यह इलाक़ा त्याग नहीं सके। नौकरी और पैसों का मोह टूट नहीं सका। मगर तू कर सकेगा, भाई, तू कर लेगा। भाग जाओ, इस नरक से भाग जाओ। हमें याद तो रहेगा कि एक आदमी था, जो किसी न किसी तरह इस नरक से भाग निकला। इस गोरखधन्धे से छुटकारा पा सका।’’
उन लोगों से विदा लेकर मैं टिफ़िन के डिब्बे-जैसी चीज़ें तक कपड़े के बैग में भरकर और कन्धे से लटकाकर बाहर निकल पड़ा। पश्चिमी आकाश का मुरझाया हुआ सूरज उस दिन मेरी ही आँखों के सामने डूब गया था।
लेकिन, इसके बाद ? उस दिन मुझे पता नहीं था कि जीवन इतना निर्मम है, पृथ्वी इतनी कठोर है, और पृथ्वी पर बसे हुए मनुष्य इतने हिसाबी हैं, अंकगणित के नियमों पर जीवन काट देते हैं। मुझे एकदम पता नहीं था।
नौकरी चाहिए। मनुष्य बनकर जीवित रहने के लिए किसी तरह भी एक नौकरी चाहिए। लेकिन नौकरी कहाँ है ? कौन देगा ?
हाथ में मैट्रिकुलेशन का सर्टिफ़िकेट लेकर कितने ही परिचितों के आगे जा खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने बड़ी ही सहानुभूति दिखलायी है। मेरे साथ घटी हुई एक आकस्मिक दुर्घटना ने उन्हें कैसा आघात पहुँचाया है, उन्होंने यह सब भी बताया है। और, नौकरी की बात सुनकर काँप गये हैं। बोलते रहे हैं, ‘‘भयानक दुर्दिन आ गया है। कम्पनी की आर्थिक अवस्था ‘हैप्पी’ नहीं है। फिर भी, कोई ‘वेकेन्सी’ हुई तो ज़रूर सूचित करके बुला लेंगे।’’
और एक दफ्तर में गया था। वहाँ के मालिक दत्त साहब एक बार बड़ी ही मुसीबत में पड़कर मेरी शरण में आये थे। मेरे ही कहने पर हमारे बैरिस्टर साहब ने फ़ीस लिये बिना ही उन्हें क़ानूनी सलाह दे दी थी।
लेकिन दत्त साहब ने तो भेंट करने से भी इन्कार कर दिया। स्लिप के साथ बैरा वापिस आ गया। साहब आज बहुत ‘बिज़ी’ हैं। भेंट नहीं कर सके, इसलिए स्लिप पर ही पेंसिल से लिखकर खेद प्रकट किया है। और संक्षेप में यह भी बता दिया है कि आगामी कई सप्ताहों तक वह इतने व्यस्त रहेंगे कि पूरी ख्वाहिश रहने पर भी मिल नहीं सकेंगे, मेरे सुमधुर सान्निध्य का उपभोग नहीं कर सकेंगे।
बैरे ने कहा था, ‘‘साहब को चिट्ठी लिखो !’’ लज्जा से चूर-चूर होते हुए मैंने चिट्ठी भी लिखी थी। कहना ज़रूरी नहीं है, उनका कोई उत्तर नहीं आया।
और भी कितने ही आवेदन-पत्र मैंने भेजे हैं। परिचितों के पास, अपरिचितों के पास, बॉक्स-नम्बरों पर, हर जगह अपनी शिक्षा-दीक्षा और गुणावली का विस्तृत विवरण उपस्थित करते हुए पत्र लिखा है। लेकिन सरकारी पोस्ट ऑफ़िस की आमदनी बढ़ाने के सिवा और कोई लाभ नहीं हुआ है।
थक गया था। चूर-चूर हो गया था। बुरे दिनों के लिए एक भी पैसा बचाकर नहीं रखा था। जो जमा-पूँजी थी, वह भी खत्म हो गयी। अब तो उपवास के सिवा कोई चारा नहीं था।
हाय भगवान् ! कलकत्ता हाईकोर्ट के अन्तिम अंग्रेज़ बैरिस्टर के अन्तिम किरानी बाबू की क़िस्मत में यही लिखा हुआ था ?
अन्त में फेरीवाले का धन्धा शुरू करना पड़ा। शिष्ट भाषा में कहेंगे—सेल्समैन ! दफ्तर-दफ्तर घूमकर ‘वेस्ट-पेपर बास्केट’ बेचना होगा। कम्पनी का नाम सुनकर तो श्रद्धा से सिर झुका लेंगे। सोचेंगे यह मैगपिल एण्ड क्लार्क कम्पनी भी बर्मा शेल, जार्डिन हेण्डर्सन, या एण्ड्रू बिल कम्पनियों की टक्कर की कोई कम्पनी है। लेकिन इस कम्पनी के कर्णधार, एम.जी. पिल्लई नाम के मद्रासी छोकरे के पास एक जोड़ा पैण्ट और एक पुरानी टाई के अलावा और कुछ पूँजी नहीं थी। छातावाला लेन के अन्धकारग्रस्त मकान की एक छोटी-सी कोठरी ही उसकी फैक्टरी थी, दफ्तर था, शो-रूम था, सोने और रसोई पकाने का एक कमरा था। एम.जी.पिल्लई ही ‘मैगपिल’ बन गया है, और क्लार्क साहब ? और कोई नहीं, मैगपिल का यह क्लर्क ही ‘क्लार्क’ है !
तार के बने हुए बास्केट मुझे बेचने होंगे ! रुपये में चार आना कमीशन मिलेगा। हर बास्केट पर चार आने ! मेरे लिए तो यही चार आने स्वर्ग की सम्पत्ति है !
फिर भी बिक्री नहीं हो पाती है। हाथ में बास्केट लिये दफ्तर-दफ्तर चक्कर काटता रहा हूँ, और मेज़ पर बैठे बाबू लोगों की कुर्सियों के नीचे झाँकता रहा हूँ। कितने लोगों ने शंकित होकर पूछा है, ‘‘वहाँ क्या देख रहे हो ?’’
मैंने उत्तर दिया है, ‘‘रद्दी कागज फेंकनेवाली टोकरी देख रहा था !’’
उनकी टोकरी फटी-पुरानी हालत में देखकर बड़ी खुशी होती थी। कहता था, आपकी टोकरी में अब कोई दम नहीं है। नया बास्केट ले लीजिए न, सर ! बहुत बढ़िया चीज़ है ! एक बास्केट रख लीजिए, दस साल के लिए निश्चिंत हो जायेंगे।’’
बड़े बाबू अपनी टोकरी की ओर दृष्टिपात करके कह देते थे, ‘‘अभी तो कण्डीशन अच्छी ही है। हँस-खेलकर साल-भर तो काट ही लेगी।’’
करुण दृष्टि से बाबू की ओर देखता हुआ खड़ा रहता था। लेकिन, मेरे मन की स्थिति वह समझ नहीं पाते थे। इच्छा होती थी, चीखकर उनसे कहूँ, ‘आपकी टोकरी हँस-खेलकर साल-भर काट ले सकती है, लेकिन मैं ? मैं तो अब एक दिन भी काट नहीं पाऊँगा, न हँस-बोलकर और न रोकर !’’
लेकिन बोलने की इच्छा होने पर भी चार्नक साहब के इस अजीबो-ग़रीब शहर में हर बात बोली नहीं जा सकती ! इसलिए हर दफ्तर से चुपचाप निकल आता रहा हूँ।
सूट में जकड़े हुए, टाई में बँधे हुए बंगाली साहबों से भी मिला हूँ। जूते का अँगूठा हिलाते-हिलाते वे बोले, ‘‘वेरी गुड ! यंग बंगाली लड़के अब बिज़नेस-लाइन में एण्टर कर रहे हैं, यह तो बड़ी ही होपफुल बात है।’’
मैंने कहा है, ‘‘अच्छा, तो आपको कितने बास्केट दे दूँ, सर ?’’
सर ने मेरी और देखकर ज़रा भी झिझके-शरमाये बिना कहा, ‘‘मुझे छः बास्केट की जरूरत है। लेकिन देखो भाई, हमारे शेयर की बात मत भूल जाना !’’
छः बास्केट की बिक्री से मुझे कुल डेढ़ रुपये का फ़ायदा है। बास्केटों की कीमत पा जाने पर, वही डेढ़ रुपया हाथ में लेकर बोला हूँ, ‘‘छः बास्केटों में मुझे कुल डेढ़ रुपया मिलता है, सर ! आप जैसा उचित समझें, ले लें।’’
सिगरेट का कश खींचते-खींचते साहब ने कहा है, ‘‘किसी दूसरे से पर्चेज करता तो ईज़ीली थर्टी परसेन्ट ले लेता। जो भी हो, आप बंगाली हैं, आपसे ट्वेण्टी फाइव ही ले रहा हूँ।’’ और इतना कहकर डेढ़ रुपये की पूरी रक़म उन्होंने मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में रख ली है। और इसके बाद दुःख प्रकट करने लगे हैं, ‘‘हमारी जाति में अब ज़रा भी ऑनेस्टी नहीं बच गयी है ! आप तो एक्सपर्ट हो गये हैं, ‘‘बिज़नेस सीख लिया है ! मगर, यह कहने का साहस कैसे हुआ कि छः टोकरियों में आपको कुल डेढ़ रुपया ही बचता है ? हम क्या घास चरते हैं ?’’
बिना कोई जवाब-सवाल किये मैं बाहर निकल आता हूँ। अवाक् होकर इस विचित्र दुनिया को समझने की कोशिश करता रहा हूँ।
आश्चर्य ! यही दुनिया एक दिन मुझे कितनी खूबसूरत लगती थी। इसी दुनिया में मैं एक दिन मनुष्य को श्रद्धा करता था। विश्वास करता था, मनुष्य के अन्दर ही देवता निवास करते हैं। अब अचानक मुझे महसूस हुआ, मैं गधा हूँ। दुनिया ने मुझे इतनी ठोकरें लगायी हैं, और मुझे होश नहीं आया है। मेरे ज्ञान-नेत्र क्या कभी खुलेंगे ही नहीं ? नहीं, नहीं, इस तरह ज़िंन्दगी नहीं चलेगी ! मुझे भी चालाक बनना पड़ेगा ! दुनियावालों की तरह अक़्लमन्द होना पड़ेगा !
वाक़ई मैं चालाक हो गया। एक रुपये की टोकरी की क़ीमत सवा रुपया बोलने लगा हूँ। जिन्होंने अपने दफ्तर के लिए टोकरी खरीदी है, बिना किसी लाज-शरम के उन्हें चार आना देकर कहा है, ‘‘इतना कम्पटीशन चल रहा है, सर ! कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बाज़ार में टिके रहने के लिए एकदम विदाउट मार्जिन बिज़नेस कर रहा हूँ !’’
मनुष्य के प्रति अपना सारा विश्वास खो बैठा हूँ, मगर इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल ऐसा लगता रहा है, स्वार्थ से अन्धी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ ! और, मुझे अपनी अक्ल से, चालाकी से जीना होगा, अपने लिए रास्ता बनाना होगा, और आगे बढ़ते जाना होगा ! जीवन के किसी उत्सव समारोह में हमें आदरणीय अतिथि का सम्मान नहीं मिलेगा, इसीलिए ज़ोर ज़बरदस्ती से हमें उत्सव में शामिल होना पड़ेगा, अपना हिस्सा माँगना पड़ेगा।
उन्हीं दिनों एक बार डलहौजी स्क्वायर के एक दफ्तर में गया था।
मई महीने का कलकत्ता ! सड़क का पिच तक पिघल रहा है। भरी दोपहरी में रास्ते आधी रात की तरह सूनसान हैं। सिर्फ़ मेरे-जैसे कुछ अभागे इस वक़्त भी यहाँ वहाँ जा रहे हैं। इन्हें किसी तरह रोका नहीं जा सकता। ये लोग इस दफ्तर से उस दफ्तर जायेंगे, और उस दफ्तर से इस दफ्तर आयेंगे, शायद कहीं कोई बात बन जाये।
पसीने से कमीज भीग गयी थी, जैसे अभी-अभी डलहौजी के लाल तालाब में डुबकी लगाकर बाहर आया हूँ। प्यास से छाती फटी जा रही है। सड़कों के किनारे घोड़ों के लिए पानी की सुव्यवस्था रहती है, मगर हमारे लिए नहीं। बेकार के कष्ट दूर करने का काम तो ‘पशु कष्ट-निवारण समिति’ का नहीं है, फिर उन्हें दोष क्यों दूँ !
एक बड़ी बिल्डिंग देखकर अन्दर घुस पड़ा। सामने ही लिफ्ट है। लिफ्ट में घुसकर हाँफने लगता हूँ। गेट बन्द करके लिफ्टमैन ने हैण्डिल घुमा दिया। लेकिन, अचानक मेरे हाथों में पड़े दो बास्केटों पर उसकी नजर पड़ गयी। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा। अनुभवी लिफ्टमैन को समझने में देर नहीं लगी कि मैं कौन हूँ ! इसलिए, दुबारा हैण्डिल घुमाया, और लिफ्ट अपनी जगह वापस आ गयी।
अँगुली से सीढ़ियों का रास्ता बताकर उसने मुझे लिफ्ट से निकाल दिया। निकालने से पहले उसने बता दिया था, ‘‘यह लिफ्ट सिर्फ़ साहबों और बाबुओं के लिए है। तुम्हारे-जैसे नवाब बहादुरों की सेवा के लिए कम्पनी मुझे तनख्वाह नहीं देती है !’’ उसने कहा था।
सच तो यह है, मेरे-जैसे फेरीवाले के लिए लिफ्ट क्यों होगी ? हमारे लिए तो पक्की सीढ़ियाँ, एक-एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जाना होगा।
यही किया है। कोई फ़रियाद नहीं की, कोई शिकायत नहीं, अपनी क़िस्मत का रोना भी नहीं। तय किया, संसार का यही नियम है। ऊपर चढ़ने की लिफ्ट सबके लिए नहीं है।
आज का दिन ही खराब है। एक टोकरी भी नहीं बिकी। मुफ्त में तीन आने खर्च हो गये। एक आना ट्राम के सेकैण्ड क्लास का किराया, एक आने का आलू-चना। इसके बाद जीभ की लालच रोक नहीं पाया। बेफ़िक्र होकर एक आने के गोलगप्पे भी ले ही लिये। यह बड़ा ग़लत काम हो गया। एक क्षण की कमजोरी ने पूरा आना उड़ा दिया !
दफ्तर में घुसकर टेबुलों के नीचे झाँकने लगा। सारी टेबुलों के नीचे टोकरी रखी हैं। दरवाजे के पास एक मेम साहब बैठी काम कर रही थीं। मुझे देखकर विरक्त स्वर में पूछने लगीं, ‘‘क्या चाहिए ?’’
मैंने कहा, ‘‘वेस्ट-पेपर-बास्केट ! वेरी गुड, मैडम ! वेरी स्ट्रांग, एण्ड वेरी-वेरी ड्यूरेबुल !’’
लेकिन यह वक्तृता काम नहीं आयी। मेम साहब ने भगा दिया। किसी तरह अपने दोनों पाँवों को खिसकाता हुआ मैं बाहर चला आया।
दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठकर बड़ी-बड़ी मूँछोंवाला एक दरबान सुरती बना रहा था। सिर पर बड़ी-सी पगड़ी। सफ़ेद ड्रेस। छाती के पास पीतल की तख्ती पर कम्पनी का नाम चमक रहा था।
दरबानजी ने मुझे पास बुलाया। पूछने लगे, ‘‘एक टोकरी बेचने से मुझे कितना बचता है। मैं समझ गया, दरबानजी आग्रहशील हैं। कहा, ‘‘कुल चार आने बचते हैं !’’
दरबानजी ने बास्केट का दाम पूछा। इस बार मैंने बेवकूफ़ी नहीं की। साफ़-साफ़ बोला, सवा रुपया।’’
बास्केट मुझसे लेकर दरबानजी दफ्तर के भीतर चले गये। मेम साहब ने कहा, ‘‘मैं तो बोल चुकी हूँ, बास्केट की जरूरत नहीं है !’’ दरबानजी, मगर छोड़ने वाले जीव नहीं हैं। तुरन्त ही बोल उठे, ‘घोष बाबू के पास टोकरी नहीं है। मित्तिर बाबू की टोकरी टूट गयी है। बड़े साहब के बास्केट का भी रंग उखड़ गया है। फिर स्टॉक में भी तो दो-चार टोकरी रखना ही चाहिए !’’
अन्त में, मेम साहब को हार माननी ही पड़ी। मुझे एक साथ छः बास्केटों का आर्डर मिल गया।
लगभग दौड़ता हुआ मैं छातावाला लेन चला आया। आधा दर्जन टोकरियाँ एक साथ बाँधकर, सिर पर उठाये मैं दफ्तर आ गया। दरबानजी बाहर ही बैठे थे। मुझे देखकर मुस्कराये।
टोकरियाँ स्टॉक में भेजकर, मेम साहब ने कहा, ‘‘रुपये तो आज नहीं मिलेंगे ! बिल बनाना होगा।’’
लौटा आ रहा था। दरबानजी ने गेट पर पकड़ लिया, ‘‘रुपया मिला ?’’
शायद सोच रहे हों, मैं उनका हिस्सा दिये बिना ही भागा जा रहा हूँ। मैंने कहा, ‘‘आज नहीं मिलेगा !’’
‘‘काहे ?’’ दरबानजी फिर उठ खड़े हुए। सीधे मेम साहब की टेबुल पर चले गये। बातचीत में अक्लमंद हैं दरबानजी। बोले, ‘‘मेम साहब, ग़रीब आदमी है। दफ्तर-दफ्तर घूमना पड़ता है....!’’
मुझे बुलाया गया। दरबानजी ने वीर-दर्प में भरकर कहा, ‘‘पेमेण्ट करवा दिया !’’ वाउचर का एक स्लिप मेरी ओर बढ़ाकर दरबानजी ने पूछा कि मैं दस्तखत करना जानता हूँ या नहीं ! दस्तखत करना नहीं आता हो तो अँगूठे का निशान लगाना होगा।
मुझे अंग्रेजी में दस्तखत करते देखकर दरबानजी ने मज़ाक किया, ‘‘आरे बाप, तुमने तो अंग्रेजी में दस्तखत मार दिया !’’
रुपये लेकर मैं बाहर आ गया। मैं दरबानों को जानता हूँ। इन्हें कमीशन का हिस्सा देना होगा। मैं पहले से ही ठीक कर चुका था।
दरबानजी ने मेरे चेहरे की ओर देखा। मैं तैयार ही था। डेढ़ रुपया उनकी ओर बढ़ाता हुआ बोला, ‘‘यही मेरा कमीशन बनता है। इसमें से जो लेना हो....’’
ऐसा भी हो सकता है, यह मुझे पता नहीं था। दरबानजी के पूरे चेहरे पर जैसे स्याही के छींटे पड़ गये हों। मुझे स्पष्ट स्मरण है विशाल वट-वृक्ष की तरह उनका दीर्घ शरीर अचानक काँपने लगा। क्रोध से, अपमान से समूचा चेहरा सिकुड़ उठा।
मैंने सोचा, इतना कम हिस्सा उन्हें पसन्द नहीं आया है, और लेना चाहते हैं। मैं कहने ही जा रहा था, ‘‘विश्वास कीजिए, दरबानजी, छः टोकरियों में मुझे डेड़ रुपये से एक पैसा ज्यादा नहीं मिलता है।’’
मगर मेरा भ्रम टूट गया। मैंने सुना, दरबानजी कह रहे थे, तुमने क्या समझा ?’’
दरबानजी को मैंने गलत समझा है। ‘‘क्या समझा तुम ? तुमको बुलाकर हमें दुःख हुआ...तुमने क्या समझा है ? पैसे के वास्ते हमने तुम्हारी टोकरी बेच दी है ? राम-राम !’’
उस दिन मैं अपनी आँखों के आँसू रोक नहीं सका था। पृथ्वी अब भी सम्पूर्णतः दयाहीन नहीं हुई है। दरबानजी की तरह लोग अब भी बचे हुए हैं।
क्या मैं आप लोगों को अब तक याद हूँ ? बहुत दिनों पहले का सुन्दर एक अपरिपक्व-बुद्धि बालक अपने विभूति भाई का हाथ पकड़कर रामकृष्णपुर घाट से ‘अम्बा’ स्टीमर पर गंगा पार करके कलकत्ता हाईकोर्ट देखने आया था। 1अंग्रेज़ बैरिस्टर साहब के पास उसे नौकरी मिल गयी थी। उनका प्यार भी मिला था। जज, बैरिस्टर मुवक्किल—सबका स्नेह सत्कार पाकर वह प्राणपण से किरानीगिरी कर सका था, और चकित आँखों से, विस्मित दृष्टि से इस अपरिचित-अनजान दुनिया के रूप, रस, गन्धों का उपभोग कर सका था।
दुःख और दरिद्रता की अन्तहीन मरुभूमि में अचानक संसार-प्रेमी विदेशी बैरिस्टर के उपवन का आश्रय पाकर मेरी भूखी और थकी हुई आत्मा अपने सारे अतीत को भूल गई थी। मैं सोचने लगा था,
-----------------------------------------------------
1लेखक के उपन्यास ‘कितने अनजान रे’ का आरम्भिक प्रसंग।
शायद यह आश्रय कभी टूटेगा नहीं, चिरकाल तक स्थायी रहेगा। लेकिन लगता है, विधाता के सतर्क, चतुर ऑडीटरों की जमात हिसाब-किताब की गलतियाँ पकड़ने के लिए हमेशा घूमती-भागती रहती है। मेरे हिसाब की गलती पकड़ने में भी उन्हें जरा-सी देर न हुई। बैरिस्टर साहब का देहान्त हो गया, और मरुभूमि का वह ‘ओसिस’ जलकर राख हो गया। मरुभूमि में गढ़ा हुआ हमारा तम्बू रेगिस्तानी हवा के एक ही झोंके से उड़ गया। पता नहीं, कहाँ चला गया। ‘फिर से चलना शुरू करो ! फॉरवर्ड मार्च !’ विजय विधाता के हृदयहीन सेनापति ने इस हारे हुए कैदी को आज्ञा दी। आत्मा गवाही नहीं देती थी, फिर भी तरह-तरह के आघातों से क्षत-विक्षत हो गये अपने मन को, अपने थके हुए, टूटे हुए शरीर की रेलगाड़ी पर चढ़ाकर आगे बढ़ाना ही पड़ा। यात्रा शुरू करनी ही पड़ी। ‘आगे बढ़ो ! पीछे की ओर मत देखो !’
मेरे सामने सूनसान रास्ता है, और मेरे पीछे सूनसान रास्ता है। लगता है, रात के अँधेरे में मैं ओल्ड पोस्ट ऑफ़िस स्ट्रीट की अनजानी और पुरानी सराय में टिक गया था। अब सुबह की रोशनी में फिर सड़क पर उतर आया हूँ। हाईकोर्ट के बाबू लोग मुझे देखने आये थे। सहानुभूति दरसा गये थे। छोका भाई ने कहा था, ‘‘उफ़, इसी उम्र में अपना मालिक खो बैठे हो, अपना घर तोड़ बैठे हो ! इतनी कच्ची उम्र में !’’
लेकिन, मैं रोया नहीं था। एक बूँद भी आँसू मेरी आँखों से नहीं टपका। इस वज्राघात से जैसे मेरी आँखों का सारा पानी धुआँ बनकर उड़ गया था।
छोका भाई ने पास बुलाकर बिठाया था। सरदारजी की दुकान से चाय मँगा ली थी। बोले थे, ‘‘समझता हूँ भाई, सब समझता हूँ। मगर, यह पापी पेट कुछ करने नहीं देता, कुछ समझने नहीं देता। देखो, जो कुछ भी मिले, उसे ग्रहण करो। पेट भरते रहो, तभी जीवित रह सकोगे। शरीर को बल मिलेगा।’’
ओल्ड पोस्ट ऑफ़िस स्ट्रीट में मैं आखिरी बार चाय पी रहा था। फिर कभी उधर जा ही नहीं पाया। यों छोका भाई ने कहा जरूर था, ‘‘चिन्ता मत करो। इसी इलाके में तुम्हारा कुछ-न-कुछ इन्तज़ाम हो जायेगा। कौन साहब ऐसा है, जो तुम्हारे जैसे किरानी को नौकरी देना नहीं चाहेगा ! हाँ, यह बात जरूर है कि एक बीवी के रहते दूसरी बीवी बुला लेना...! हर साहब के पास कोई-न-कोई किरानी तो है ही।’’
किसी बात पर जोर देना, किसी पर दबाव डालना मेरे स्वभाव के विपरीत है। मगर, उस दिन मैं चुप नहीं रह सका था। पूरी ताक़त से मैंने कहा था, ‘‘छोका भाई, मुझसे नहीं होगा। नौकरी मिल भी जाये, मगर, अब इस मुहल्ले में रहना मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगा।’’
छोका भाई, अर्जुन भाई, हारू भाई, उस दिन सभी व्यक्ति मेरे दुःख से अभीभूत हो गये थे। विषण्ण होकर छोका भाई ने कहा था, ‘‘हम लोग तो यह इलाक़ा त्याग नहीं सके। नौकरी और पैसों का मोह टूट नहीं सका। मगर तू कर सकेगा, भाई, तू कर लेगा। भाग जाओ, इस नरक से भाग जाओ। हमें याद तो रहेगा कि एक आदमी था, जो किसी न किसी तरह इस नरक से भाग निकला। इस गोरखधन्धे से छुटकारा पा सका।’’
उन लोगों से विदा लेकर मैं टिफ़िन के डिब्बे-जैसी चीज़ें तक कपड़े के बैग में भरकर और कन्धे से लटकाकर बाहर निकल पड़ा। पश्चिमी आकाश का मुरझाया हुआ सूरज उस दिन मेरी ही आँखों के सामने डूब गया था।
लेकिन, इसके बाद ? उस दिन मुझे पता नहीं था कि जीवन इतना निर्मम है, पृथ्वी इतनी कठोर है, और पृथ्वी पर बसे हुए मनुष्य इतने हिसाबी हैं, अंकगणित के नियमों पर जीवन काट देते हैं। मुझे एकदम पता नहीं था।
नौकरी चाहिए। मनुष्य बनकर जीवित रहने के लिए किसी तरह भी एक नौकरी चाहिए। लेकिन नौकरी कहाँ है ? कौन देगा ?
हाथ में मैट्रिकुलेशन का सर्टिफ़िकेट लेकर कितने ही परिचितों के आगे जा खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने बड़ी ही सहानुभूति दिखलायी है। मेरे साथ घटी हुई एक आकस्मिक दुर्घटना ने उन्हें कैसा आघात पहुँचाया है, उन्होंने यह सब भी बताया है। और, नौकरी की बात सुनकर काँप गये हैं। बोलते रहे हैं, ‘‘भयानक दुर्दिन आ गया है। कम्पनी की आर्थिक अवस्था ‘हैप्पी’ नहीं है। फिर भी, कोई ‘वेकेन्सी’ हुई तो ज़रूर सूचित करके बुला लेंगे।’’
और एक दफ्तर में गया था। वहाँ के मालिक दत्त साहब एक बार बड़ी ही मुसीबत में पड़कर मेरी शरण में आये थे। मेरे ही कहने पर हमारे बैरिस्टर साहब ने फ़ीस लिये बिना ही उन्हें क़ानूनी सलाह दे दी थी।
लेकिन दत्त साहब ने तो भेंट करने से भी इन्कार कर दिया। स्लिप के साथ बैरा वापिस आ गया। साहब आज बहुत ‘बिज़ी’ हैं। भेंट नहीं कर सके, इसलिए स्लिप पर ही पेंसिल से लिखकर खेद प्रकट किया है। और संक्षेप में यह भी बता दिया है कि आगामी कई सप्ताहों तक वह इतने व्यस्त रहेंगे कि पूरी ख्वाहिश रहने पर भी मिल नहीं सकेंगे, मेरे सुमधुर सान्निध्य का उपभोग नहीं कर सकेंगे।
बैरे ने कहा था, ‘‘साहब को चिट्ठी लिखो !’’ लज्जा से चूर-चूर होते हुए मैंने चिट्ठी भी लिखी थी। कहना ज़रूरी नहीं है, उनका कोई उत्तर नहीं आया।
और भी कितने ही आवेदन-पत्र मैंने भेजे हैं। परिचितों के पास, अपरिचितों के पास, बॉक्स-नम्बरों पर, हर जगह अपनी शिक्षा-दीक्षा और गुणावली का विस्तृत विवरण उपस्थित करते हुए पत्र लिखा है। लेकिन सरकारी पोस्ट ऑफ़िस की आमदनी बढ़ाने के सिवा और कोई लाभ नहीं हुआ है।
थक गया था। चूर-चूर हो गया था। बुरे दिनों के लिए एक भी पैसा बचाकर नहीं रखा था। जो जमा-पूँजी थी, वह भी खत्म हो गयी। अब तो उपवास के सिवा कोई चारा नहीं था।
हाय भगवान् ! कलकत्ता हाईकोर्ट के अन्तिम अंग्रेज़ बैरिस्टर के अन्तिम किरानी बाबू की क़िस्मत में यही लिखा हुआ था ?
अन्त में फेरीवाले का धन्धा शुरू करना पड़ा। शिष्ट भाषा में कहेंगे—सेल्समैन ! दफ्तर-दफ्तर घूमकर ‘वेस्ट-पेपर बास्केट’ बेचना होगा। कम्पनी का नाम सुनकर तो श्रद्धा से सिर झुका लेंगे। सोचेंगे यह मैगपिल एण्ड क्लार्क कम्पनी भी बर्मा शेल, जार्डिन हेण्डर्सन, या एण्ड्रू बिल कम्पनियों की टक्कर की कोई कम्पनी है। लेकिन इस कम्पनी के कर्णधार, एम.जी. पिल्लई नाम के मद्रासी छोकरे के पास एक जोड़ा पैण्ट और एक पुरानी टाई के अलावा और कुछ पूँजी नहीं थी। छातावाला लेन के अन्धकारग्रस्त मकान की एक छोटी-सी कोठरी ही उसकी फैक्टरी थी, दफ्तर था, शो-रूम था, सोने और रसोई पकाने का एक कमरा था। एम.जी.पिल्लई ही ‘मैगपिल’ बन गया है, और क्लार्क साहब ? और कोई नहीं, मैगपिल का यह क्लर्क ही ‘क्लार्क’ है !
तार के बने हुए बास्केट मुझे बेचने होंगे ! रुपये में चार आना कमीशन मिलेगा। हर बास्केट पर चार आने ! मेरे लिए तो यही चार आने स्वर्ग की सम्पत्ति है !
फिर भी बिक्री नहीं हो पाती है। हाथ में बास्केट लिये दफ्तर-दफ्तर चक्कर काटता रहा हूँ, और मेज़ पर बैठे बाबू लोगों की कुर्सियों के नीचे झाँकता रहा हूँ। कितने लोगों ने शंकित होकर पूछा है, ‘‘वहाँ क्या देख रहे हो ?’’
मैंने उत्तर दिया है, ‘‘रद्दी कागज फेंकनेवाली टोकरी देख रहा था !’’
उनकी टोकरी फटी-पुरानी हालत में देखकर बड़ी खुशी होती थी। कहता था, आपकी टोकरी में अब कोई दम नहीं है। नया बास्केट ले लीजिए न, सर ! बहुत बढ़िया चीज़ है ! एक बास्केट रख लीजिए, दस साल के लिए निश्चिंत हो जायेंगे।’’
बड़े बाबू अपनी टोकरी की ओर दृष्टिपात करके कह देते थे, ‘‘अभी तो कण्डीशन अच्छी ही है। हँस-खेलकर साल-भर तो काट ही लेगी।’’
करुण दृष्टि से बाबू की ओर देखता हुआ खड़ा रहता था। लेकिन, मेरे मन की स्थिति वह समझ नहीं पाते थे। इच्छा होती थी, चीखकर उनसे कहूँ, ‘आपकी टोकरी हँस-खेलकर साल-भर काट ले सकती है, लेकिन मैं ? मैं तो अब एक दिन भी काट नहीं पाऊँगा, न हँस-बोलकर और न रोकर !’’
लेकिन बोलने की इच्छा होने पर भी चार्नक साहब के इस अजीबो-ग़रीब शहर में हर बात बोली नहीं जा सकती ! इसलिए हर दफ्तर से चुपचाप निकल आता रहा हूँ।
सूट में जकड़े हुए, टाई में बँधे हुए बंगाली साहबों से भी मिला हूँ। जूते का अँगूठा हिलाते-हिलाते वे बोले, ‘‘वेरी गुड ! यंग बंगाली लड़के अब बिज़नेस-लाइन में एण्टर कर रहे हैं, यह तो बड़ी ही होपफुल बात है।’’
मैंने कहा है, ‘‘अच्छा, तो आपको कितने बास्केट दे दूँ, सर ?’’
सर ने मेरी और देखकर ज़रा भी झिझके-शरमाये बिना कहा, ‘‘मुझे छः बास्केट की जरूरत है। लेकिन देखो भाई, हमारे शेयर की बात मत भूल जाना !’’
छः बास्केट की बिक्री से मुझे कुल डेढ़ रुपये का फ़ायदा है। बास्केटों की कीमत पा जाने पर, वही डेढ़ रुपया हाथ में लेकर बोला हूँ, ‘‘छः बास्केटों में मुझे कुल डेढ़ रुपया मिलता है, सर ! आप जैसा उचित समझें, ले लें।’’
सिगरेट का कश खींचते-खींचते साहब ने कहा है, ‘‘किसी दूसरे से पर्चेज करता तो ईज़ीली थर्टी परसेन्ट ले लेता। जो भी हो, आप बंगाली हैं, आपसे ट्वेण्टी फाइव ही ले रहा हूँ।’’ और इतना कहकर डेढ़ रुपये की पूरी रक़म उन्होंने मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में रख ली है। और इसके बाद दुःख प्रकट करने लगे हैं, ‘‘हमारी जाति में अब ज़रा भी ऑनेस्टी नहीं बच गयी है ! आप तो एक्सपर्ट हो गये हैं, ‘‘बिज़नेस सीख लिया है ! मगर, यह कहने का साहस कैसे हुआ कि छः टोकरियों में आपको कुल डेढ़ रुपया ही बचता है ? हम क्या घास चरते हैं ?’’
बिना कोई जवाब-सवाल किये मैं बाहर निकल आता हूँ। अवाक् होकर इस विचित्र दुनिया को समझने की कोशिश करता रहा हूँ।
आश्चर्य ! यही दुनिया एक दिन मुझे कितनी खूबसूरत लगती थी। इसी दुनिया में मैं एक दिन मनुष्य को श्रद्धा करता था। विश्वास करता था, मनुष्य के अन्दर ही देवता निवास करते हैं। अब अचानक मुझे महसूस हुआ, मैं गधा हूँ। दुनिया ने मुझे इतनी ठोकरें लगायी हैं, और मुझे होश नहीं आया है। मेरे ज्ञान-नेत्र क्या कभी खुलेंगे ही नहीं ? नहीं, नहीं, इस तरह ज़िंन्दगी नहीं चलेगी ! मुझे भी चालाक बनना पड़ेगा ! दुनियावालों की तरह अक़्लमन्द होना पड़ेगा !
वाक़ई मैं चालाक हो गया। एक रुपये की टोकरी की क़ीमत सवा रुपया बोलने लगा हूँ। जिन्होंने अपने दफ्तर के लिए टोकरी खरीदी है, बिना किसी लाज-शरम के उन्हें चार आना देकर कहा है, ‘‘इतना कम्पटीशन चल रहा है, सर ! कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बाज़ार में टिके रहने के लिए एकदम विदाउट मार्जिन बिज़नेस कर रहा हूँ !’’
मनुष्य के प्रति अपना सारा विश्वास खो बैठा हूँ, मगर इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल ऐसा लगता रहा है, स्वार्थ से अन्धी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ ! और, मुझे अपनी अक्ल से, चालाकी से जीना होगा, अपने लिए रास्ता बनाना होगा, और आगे बढ़ते जाना होगा ! जीवन के किसी उत्सव समारोह में हमें आदरणीय अतिथि का सम्मान नहीं मिलेगा, इसीलिए ज़ोर ज़बरदस्ती से हमें उत्सव में शामिल होना पड़ेगा, अपना हिस्सा माँगना पड़ेगा।
उन्हीं दिनों एक बार डलहौजी स्क्वायर के एक दफ्तर में गया था।
मई महीने का कलकत्ता ! सड़क का पिच तक पिघल रहा है। भरी दोपहरी में रास्ते आधी रात की तरह सूनसान हैं। सिर्फ़ मेरे-जैसे कुछ अभागे इस वक़्त भी यहाँ वहाँ जा रहे हैं। इन्हें किसी तरह रोका नहीं जा सकता। ये लोग इस दफ्तर से उस दफ्तर जायेंगे, और उस दफ्तर से इस दफ्तर आयेंगे, शायद कहीं कोई बात बन जाये।
पसीने से कमीज भीग गयी थी, जैसे अभी-अभी डलहौजी के लाल तालाब में डुबकी लगाकर बाहर आया हूँ। प्यास से छाती फटी जा रही है। सड़कों के किनारे घोड़ों के लिए पानी की सुव्यवस्था रहती है, मगर हमारे लिए नहीं। बेकार के कष्ट दूर करने का काम तो ‘पशु कष्ट-निवारण समिति’ का नहीं है, फिर उन्हें दोष क्यों दूँ !
एक बड़ी बिल्डिंग देखकर अन्दर घुस पड़ा। सामने ही लिफ्ट है। लिफ्ट में घुसकर हाँफने लगता हूँ। गेट बन्द करके लिफ्टमैन ने हैण्डिल घुमा दिया। लेकिन, अचानक मेरे हाथों में पड़े दो बास्केटों पर उसकी नजर पड़ गयी। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा। अनुभवी लिफ्टमैन को समझने में देर नहीं लगी कि मैं कौन हूँ ! इसलिए, दुबारा हैण्डिल घुमाया, और लिफ्ट अपनी जगह वापस आ गयी।
अँगुली से सीढ़ियों का रास्ता बताकर उसने मुझे लिफ्ट से निकाल दिया। निकालने से पहले उसने बता दिया था, ‘‘यह लिफ्ट सिर्फ़ साहबों और बाबुओं के लिए है। तुम्हारे-जैसे नवाब बहादुरों की सेवा के लिए कम्पनी मुझे तनख्वाह नहीं देती है !’’ उसने कहा था।
सच तो यह है, मेरे-जैसे फेरीवाले के लिए लिफ्ट क्यों होगी ? हमारे लिए तो पक्की सीढ़ियाँ, एक-एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जाना होगा।
यही किया है। कोई फ़रियाद नहीं की, कोई शिकायत नहीं, अपनी क़िस्मत का रोना भी नहीं। तय किया, संसार का यही नियम है। ऊपर चढ़ने की लिफ्ट सबके लिए नहीं है।
आज का दिन ही खराब है। एक टोकरी भी नहीं बिकी। मुफ्त में तीन आने खर्च हो गये। एक आना ट्राम के सेकैण्ड क्लास का किराया, एक आने का आलू-चना। इसके बाद जीभ की लालच रोक नहीं पाया। बेफ़िक्र होकर एक आने के गोलगप्पे भी ले ही लिये। यह बड़ा ग़लत काम हो गया। एक क्षण की कमजोरी ने पूरा आना उड़ा दिया !
दफ्तर में घुसकर टेबुलों के नीचे झाँकने लगा। सारी टेबुलों के नीचे टोकरी रखी हैं। दरवाजे के पास एक मेम साहब बैठी काम कर रही थीं। मुझे देखकर विरक्त स्वर में पूछने लगीं, ‘‘क्या चाहिए ?’’
मैंने कहा, ‘‘वेस्ट-पेपर-बास्केट ! वेरी गुड, मैडम ! वेरी स्ट्रांग, एण्ड वेरी-वेरी ड्यूरेबुल !’’
लेकिन यह वक्तृता काम नहीं आयी। मेम साहब ने भगा दिया। किसी तरह अपने दोनों पाँवों को खिसकाता हुआ मैं बाहर चला आया।
दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठकर बड़ी-बड़ी मूँछोंवाला एक दरबान सुरती बना रहा था। सिर पर बड़ी-सी पगड़ी। सफ़ेद ड्रेस। छाती के पास पीतल की तख्ती पर कम्पनी का नाम चमक रहा था।
दरबानजी ने मुझे पास बुलाया। पूछने लगे, ‘‘एक टोकरी बेचने से मुझे कितना बचता है। मैं समझ गया, दरबानजी आग्रहशील हैं। कहा, ‘‘कुल चार आने बचते हैं !’’
दरबानजी ने बास्केट का दाम पूछा। इस बार मैंने बेवकूफ़ी नहीं की। साफ़-साफ़ बोला, सवा रुपया।’’
बास्केट मुझसे लेकर दरबानजी दफ्तर के भीतर चले गये। मेम साहब ने कहा, ‘‘मैं तो बोल चुकी हूँ, बास्केट की जरूरत नहीं है !’’ दरबानजी, मगर छोड़ने वाले जीव नहीं हैं। तुरन्त ही बोल उठे, ‘घोष बाबू के पास टोकरी नहीं है। मित्तिर बाबू की टोकरी टूट गयी है। बड़े साहब के बास्केट का भी रंग उखड़ गया है। फिर स्टॉक में भी तो दो-चार टोकरी रखना ही चाहिए !’’
अन्त में, मेम साहब को हार माननी ही पड़ी। मुझे एक साथ छः बास्केटों का आर्डर मिल गया।
लगभग दौड़ता हुआ मैं छातावाला लेन चला आया। आधा दर्जन टोकरियाँ एक साथ बाँधकर, सिर पर उठाये मैं दफ्तर आ गया। दरबानजी बाहर ही बैठे थे। मुझे देखकर मुस्कराये।
टोकरियाँ स्टॉक में भेजकर, मेम साहब ने कहा, ‘‘रुपये तो आज नहीं मिलेंगे ! बिल बनाना होगा।’’
लौटा आ रहा था। दरबानजी ने गेट पर पकड़ लिया, ‘‘रुपया मिला ?’’
शायद सोच रहे हों, मैं उनका हिस्सा दिये बिना ही भागा जा रहा हूँ। मैंने कहा, ‘‘आज नहीं मिलेगा !’’
‘‘काहे ?’’ दरबानजी फिर उठ खड़े हुए। सीधे मेम साहब की टेबुल पर चले गये। बातचीत में अक्लमंद हैं दरबानजी। बोले, ‘‘मेम साहब, ग़रीब आदमी है। दफ्तर-दफ्तर घूमना पड़ता है....!’’
मुझे बुलाया गया। दरबानजी ने वीर-दर्प में भरकर कहा, ‘‘पेमेण्ट करवा दिया !’’ वाउचर का एक स्लिप मेरी ओर बढ़ाकर दरबानजी ने पूछा कि मैं दस्तखत करना जानता हूँ या नहीं ! दस्तखत करना नहीं आता हो तो अँगूठे का निशान लगाना होगा।
मुझे अंग्रेजी में दस्तखत करते देखकर दरबानजी ने मज़ाक किया, ‘‘आरे बाप, तुमने तो अंग्रेजी में दस्तखत मार दिया !’’
रुपये लेकर मैं बाहर आ गया। मैं दरबानों को जानता हूँ। इन्हें कमीशन का हिस्सा देना होगा। मैं पहले से ही ठीक कर चुका था।
दरबानजी ने मेरे चेहरे की ओर देखा। मैं तैयार ही था। डेढ़ रुपया उनकी ओर बढ़ाता हुआ बोला, ‘‘यही मेरा कमीशन बनता है। इसमें से जो लेना हो....’’
ऐसा भी हो सकता है, यह मुझे पता नहीं था। दरबानजी के पूरे चेहरे पर जैसे स्याही के छींटे पड़ गये हों। मुझे स्पष्ट स्मरण है विशाल वट-वृक्ष की तरह उनका दीर्घ शरीर अचानक काँपने लगा। क्रोध से, अपमान से समूचा चेहरा सिकुड़ उठा।
मैंने सोचा, इतना कम हिस्सा उन्हें पसन्द नहीं आया है, और लेना चाहते हैं। मैं कहने ही जा रहा था, ‘‘विश्वास कीजिए, दरबानजी, छः टोकरियों में मुझे डेड़ रुपये से एक पैसा ज्यादा नहीं मिलता है।’’
मगर मेरा भ्रम टूट गया। मैंने सुना, दरबानजी कह रहे थे, तुमने क्या समझा ?’’
दरबानजी को मैंने गलत समझा है। ‘‘क्या समझा तुम ? तुमको बुलाकर हमें दुःख हुआ...तुमने क्या समझा है ? पैसे के वास्ते हमने तुम्हारी टोकरी बेच दी है ? राम-राम !’’
उस दिन मैं अपनी आँखों के आँसू रोक नहीं सका था। पृथ्वी अब भी सम्पूर्णतः दयाहीन नहीं हुई है। दरबानजी की तरह लोग अब भी बचे हुए हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i