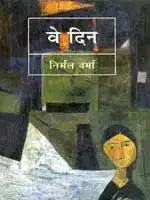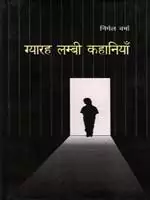|
विविध उपन्यास >> वे दिन वे दिननिर्मल वर्मा
|
373 पाठक हैं |
|||||||
इस उपन्यास के पात्र, निर्मलजी के अन्य कथा-चरित्रों की ही तरह सबसे पहले व्यक्ति है, लेकिन मनुष्य के तौर पर वे कहीं भी कम नहीं हैं बल्कि बढ़कर हैं, किसी भी मानवीय समाज के लिए उनकी मौजूदगी अपेक्षित मानी जायगी उनकी पीड़ा और उस पीड़ा को पहचानने, अंगीकार करने की उनकी इच्छा और क्षमता उन्हें हमारे मौजूद असहिष्णु समाज के लिए मूल्यवान बनाती है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
इतिहास निर्मल वर्मा के कथा-शिल्प में उसी तरह मौजूद रहता है जैसे हमारे जीवन में-लगातार मौजूद लेकिन अदृश्य। उससे हमारे दुःख और सुख तय होते हैं वैसे ही जैसे उनके कथा-पात्रों के। कहानी का विस्तार उसमें बस यह करता है कि इतिहास के उन मूक और भीड़ में अनचीन्हे ‘विषयों’ को एक आलोक-वृत्त से घेरकर नुमायाँ कर देता है, ताकि वे दिखने लगे, ताकि उनकी पीड़ा की सूचना एक जवाबी संदेश की तरह इतिहास और उसकी नियंता शक्तियों तक पहुँच सके। इस प्रक्रिया में अगर उनकी कथा कुछ ऐसे व्यक्तियों को रच देती है कि जिनकी वैयक्तिकता की आभा हमारे लिए ईर्ष्या का कारण हो उठे, तो यह उनका व्यक्तिवाद नहीं है, व्यक्ति के स्तर पर एक वैकल्पिक मनुष्य का खाका तैयार करने की कोशिश है।
इस उपन्यास के पात्र, निर्मलजी के अन्य कथा-चरित्रों की ही तरह सबसे पहले व्यक्ति है, लेकिन मनुष्य के तौर पर वे कहीं भी कम नहीं हैं बल्कि बढ़कर हैं, किसी भी मानवीय समाज के लिए उनकी मौजूदगी अपेक्षित मानी जायगी उनकी पीड़ा और उस पीड़ा को पहचानने, अंगीकार करने की उनकी इच्छा और क्षमता उन्हें हमारे मौजूद असहिष्णु समाज के लिए मूल्यवान बनाती है। वह चाहे रायना हो, इंदी हो, फ्रांज हो या मारिया, उनमें से कोई भी अपने दुख का हिसाब हर किसी से नहीं माँगता फिरता। चेकोस्लोवाकिया की बर्फ-भरी सड़कों पर अपने लगभग अपरिभाषित-से-प्रेम के साथ घूमते हुए ये पात्र जब पन्नों पर उद्घाटित होते हैं तो हमें एक टीसती हुई-सी सांत्वना प्राप्त होती है, कि मनुष्य होने का जोखिम लेने के दिन अभी लद नहीं गए।
इस उपन्यास के पात्र, निर्मलजी के अन्य कथा-चरित्रों की ही तरह सबसे पहले व्यक्ति है, लेकिन मनुष्य के तौर पर वे कहीं भी कम नहीं हैं बल्कि बढ़कर हैं, किसी भी मानवीय समाज के लिए उनकी मौजूदगी अपेक्षित मानी जायगी उनकी पीड़ा और उस पीड़ा को पहचानने, अंगीकार करने की उनकी इच्छा और क्षमता उन्हें हमारे मौजूद असहिष्णु समाज के लिए मूल्यवान बनाती है। वह चाहे रायना हो, इंदी हो, फ्रांज हो या मारिया, उनमें से कोई भी अपने दुख का हिसाब हर किसी से नहीं माँगता फिरता। चेकोस्लोवाकिया की बर्फ-भरी सड़कों पर अपने लगभग अपरिभाषित-से-प्रेम के साथ घूमते हुए ये पात्र जब पन्नों पर उद्घाटित होते हैं तो हमें एक टीसती हुई-सी सांत्वना प्राप्त होती है, कि मनुष्य होने का जोखिम लेने के दिन अभी लद नहीं गए।
वे दिन
यही समय होता था। यही घड़ी। मैं कुर्सी पर बैठा रहा करता था.....एक ठंडी-सी सिहरन को अपनी समूची देह में दबाता हुआ। सामने खिड़की थी-शीशों पर कुहरा जम गया था। मैंने रूमाल निकाला। फिर उसे आँखों पर दबाकर मेज़ पर सिर टिका लिया। मैं देर तक ठिठुरता रहा। कमरे की अंगीठी में लकड़ियाँ पड़ी थीं-सूखी अधजली। रोशनदान में फँसा पुराना अख़बार बार-बार काँपने लगता था......जैसे कोई पक्षी उड़ने के लिए बार-बार पंख फड़फड़ाता हो-और फिर असहाय-सा बैठ जाता हो।
‘‘तुम विश्वास करते हो ? सच बताओ !.....’’
वही एक आवाज़ ! हर दिन इसी घड़ी में वह मुझे पकड़ लेती थी....एक विवश आग्रह के साथ। जैसे वह दोनों हाथ से उसका चेहरा दबोच लेता था-और उसकी आतंकग्रस्त आँखें उस पर टिक जाती थीं।
सफ़ेद पुतलियों पर एक अजीब-सी जिज्ञासा सिमट आती थी।
वे अब भी यहाँ होंगी-हवा में टिमकती दो आँखें। इस क्षण और आनेवाले हर क्षण में मेरी ओर निहारती हुईं। मैंने चारों ओर देखा। पलँग के पास की दीवार पर एक मैला-सा दाग़ था-उतना ही बड़ा, जितना तकिए का बीच का हिस्सा। पहली बार मेरी दृष्टि वहाँ गई थी-यह वहाँ पहले नहीं था। उसके आने के बाद शुरु हुआ था.....पहले महज़ एक धब्बा था, फिर धीरे-
धीरे वह फैलता गया था। वह यहीं बैठा करती थी-तकिए को दीवार से सटाकर, अंगीठी से लपटों की छाया में उसका चेहरा जगता-बुझता रहता था।
मैं खिड़की के शीशों को पोंछने लगा....सामने दूसरे मकान थे, ज़र्द और पुराने। दिसम्बर की हल्की, पीली रोशनी गीले पत्थरों पर गिर रही थी। पिघली हुई बर्फ का मैला पानी दरवाजों के आगे जमा हो गया था....मैंने तपता माथा खिड़की के ठंडे आइने पर रख दिया। आँखे मुँद गईं।
सच.....क्या तुम विश्वास नहीं करते ?
अँधेरे कॉरीडोर में टेलीफोन की घंटी खड़कने लगी....अनायस सिर शीशे से ऊपर उठ गया। आतुर प्रतीक्षा में फैली मेरी आँखे बन्द दरवाज़े पर टिक गई। घंटी बजती रही....वह हॉस्टल का कॉमन टेलीफोन था, दस कमरों के कॉरीडोर के बीचोंबीच। पुरानी आदत मुझे दरवाजे के पास घसीट लाई थी। मैं कान लगाए सुन रहा था। मुझमें इतना साहस भी नहीं होता था कि स्वयं बाहर आकर रिसीवर उठा लूँ। घंटी की चीखती आवाज़ मेरी चेतना की परत को महज छू आती थी....आगे कुछ भी नहीं था। यह मैं जानता था, फिर भी मैं धीरे-धीरे काँपने लगा था। एक भयंकर थपाटे से किसी कमरे का दरवाजा़ खुला था। कॉरीडोर के पुराने फर्श पर जूतों की आवाज़....टेलीफ़ोन की ओर तेज़ी से बढ़ती हुई।
क्या यह उसका नाम है ? पहले हमेशा यही होता था.....शाम की इस घड़ी में। मैं जूते-मोज़े पहनकर बिस्तर पर लेटा रहा करता था। दोपहर से शाम की इस घड़ी की प्रतीक्षा में......टेलीफोन की घँटी बजती थी.....जूतों की आवाज़ मेरे दरवाज़े के सामने ठहर जाती थी......
रूम नम्बर 13 टेलीफ़ोन !
मैंने झपटकर दरवाजे़ का हैंडिल पकड़ लिया। दिसम्बर के इस मौसम में भी मेरी हथेलियाँ पसीने से तर थीं। किसी ने मेरा दरवाज़ा नहीं खटखटाया.....जूतों की आवाज़ मेरे दरवाज़े के निकट आई......लेकिन रुकी नहीं, केवल मेरी साँस को रोककर आगे बढ़ गई। मैं मुड़ा, और दरवाज़े से पीठ सटाकर कमरे की ओर देखने लगा।
मुझे आश्चर्य हुआ। सब-कुछ वैसा ही था-बेसिन के आले में रखा साबुन, साबुन में लिथड़ा ब्रुश, टप-टप नल की बूँदें। बाहर कॉरीडोर में अब सम्पूर्ण शान्ति थी.....सिर्फ़ हवा चलने से रोशनदान में फँसा अखबार फड़फड़ाने लगता था।
मैं दबे कदमों से आगे बढ़ा, जैसे चोरी-चुपके से किसी पराए कमरे में चले आया हूँ। अपने बिस्तर के पास आकर मेरे पाँव ठिठक गए। मैं काँपते हाथों से सिरहाने की दीवार छूने लगा......दीवार से सिर्फ उस हिस्से को, जो पीठ की रगड़ से स्याह पड़ गया था। एक लम्बी-पतली पीठ का निशान..........
‘‘सुनो !’’ अँधेरे में किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया है। मेरी काँपती अँगुलियाँ दीवार पर टिकी रहती हैं....सच बताओ....क्या तुम बिल्कुल विश्वास नहीं करते ?
यह आवाज़ उसकी है। कितनी बार उसने उसे सुना है।
लगता है, उसके चले जाने के बाद भी यह आवाज़ पीछे छूट गई थी-अपने में अलग और सम्पूर्ण। मैं खिड़की खोलता हुआ डरता हूँ......दरवाज़े पर भी कोई दस्तक देता है, तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है......लगता है, ज़रा-सा भी रास्ता पाने पर यह आवाज़ बाहर निकल जाएगी और मुझे पकड़ लेगी। मैं कब तक उसे रोक सकूँगा-अधीर-आग्रहपूर्ण, आँसुओं में भीगी उस आवाज़ को, जैसा मैंने उसे रात की अकेली घड़ी में सुना था ?
मैं देर तक कमरे की अँगीठी के सामने खड़ा रहा। सर्दी बढ़ गई थी और मैं गर्म ऊनी जैकेट के भीतर भी ठिठुर रहा था। फिर भी मैं आग जलाने की हिम्मत नहीं बटोर सका। कुहरे में ढँकी खिड़की के पीछे डाइनिंग-हॉल की बत्ती जली थी....बर्फ़ के छोटे-छोटे गाले सफ़ेद तितलियों से रोशनी को छूते हुए अँधेरे में गायब हो जाते थे।
सफ़ेद, खामोश बर्फ़।
किसी ने धीमे से दरवाज़ा खटखटाया था....मैं सो रहा था और एकदम चौंककर उठ गया। आँखें दरवाज़े पर टिक गईं।
-रूम नंबर 13...यू हैव टेलीफ़ोन ! सोते हुए मैं घंटी नहीं सुन सका था। चप्पल पहनकर कॉरीडोर में आया......इस समय मुझे कौन बुला सकता है ? क्रिसमस की छुट्टियाँ आरम्भ हो चुकी थीं और मेरे लगभग सभी मित्र प्राग से बाहर चले गए थे। मैंने रिसीवर उठाया.......एक भारी, अपरिचित स्वर सुनाई दिया, ‘‘क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं......हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।’’
‘‘अभी ?’’ मैंने हाथ पर लगी घड़ी देखी.....आठ से अधिक समय नहीं हुआ था.....मैं शाम को अचानक सो गया था और नींद अब भी मेरी अलसाई नसों पर रेंग रही थी। ‘‘क्या कल आना नहीं हो सकेगा ?’’ मैंने झिझकते हुए कहा। ‘‘कल..?’’ रिसीवर में एक क्षण तक सन्नाटा रहा...फिर वही आवाज़ सुनाई दी...इस बार बौखलाई-सी, ‘‘ईश्वर के लिए....अभी। हो सके तो टैक्सी लेकर आ जाइए....क्या आपको पता मालूम है ?’’
एक क्षण के लिए जी में आया कि मैं जाने से इनकार कर दूँ।
‘टूरिस्ट एजेन्सी’ को इस समय मुझसे क्या काम हो सकता है, मैं कोई अनुमान नहीं लगा सका।
‘‘मुझे आधा घंटा लग जाएगा।’’ मैंने कहा।
‘‘ओ के, ठीक है....हम प्रतीक्षा कर रहे हैं....हो सके तो टैक्सी ले लीजिए.....वी शैल पे फॉर इट...’’
मैंने रिसीवर रख दिया। टेलीफ़ोन के पास ही होस्टल का प्राइवेट किचन था। कुछ अरब विद्यार्थी वहाँ खड़े थे....माकरोनी और तली हुई मछली की गन्ध कॉरीडोर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल रही थी। ब्लॉक के कोने में सीढ़ियों के पास, एक नीग्रो छात्र किसी चेक लड़की से बहुत धीमे दबे स्वर में बातचीत कर रहा था। यह पुराने हास्टल की पुरानी मंज़िल थी.....यहाँ सिर्फ़ फ़ाइन-आर्ट्स के विद्यार्थी रहते थे। शाम के समय अक्सर कमरों में वायलन या सेक्सोफोन की आवाज़े सुनाई देती थीं। लेकिन छुट्टियों में होस्टल उजाड़ हो जाता.......सिवाय कुछ विदेशी छात्र आख़िर तक बने रहते।
मैं अपने कमरे में आया और फ्राइंग-पैन को स्टोव पर रख दिया। अलमारी के निचले दराज़ से प्याज़, मार्जरीन और मछली का टिन बाहर निकाला। बाउन-ब्रेड की दो कतरी हुई स्लाइसें मेज़ पर रख दी......मैं सोता रहा था और अब मुझे अचानक भूख लग आई थी।
‘‘तुम विश्वास करते हो ? सच बताओ !.....’’
वही एक आवाज़ ! हर दिन इसी घड़ी में वह मुझे पकड़ लेती थी....एक विवश आग्रह के साथ। जैसे वह दोनों हाथ से उसका चेहरा दबोच लेता था-और उसकी आतंकग्रस्त आँखें उस पर टिक जाती थीं।
सफ़ेद पुतलियों पर एक अजीब-सी जिज्ञासा सिमट आती थी।
वे अब भी यहाँ होंगी-हवा में टिमकती दो आँखें। इस क्षण और आनेवाले हर क्षण में मेरी ओर निहारती हुईं। मैंने चारों ओर देखा। पलँग के पास की दीवार पर एक मैला-सा दाग़ था-उतना ही बड़ा, जितना तकिए का बीच का हिस्सा। पहली बार मेरी दृष्टि वहाँ गई थी-यह वहाँ पहले नहीं था। उसके आने के बाद शुरु हुआ था.....पहले महज़ एक धब्बा था, फिर धीरे-
धीरे वह फैलता गया था। वह यहीं बैठा करती थी-तकिए को दीवार से सटाकर, अंगीठी से लपटों की छाया में उसका चेहरा जगता-बुझता रहता था।
मैं खिड़की के शीशों को पोंछने लगा....सामने दूसरे मकान थे, ज़र्द और पुराने। दिसम्बर की हल्की, पीली रोशनी गीले पत्थरों पर गिर रही थी। पिघली हुई बर्फ का मैला पानी दरवाजों के आगे जमा हो गया था....मैंने तपता माथा खिड़की के ठंडे आइने पर रख दिया। आँखे मुँद गईं।
सच.....क्या तुम विश्वास नहीं करते ?
अँधेरे कॉरीडोर में टेलीफोन की घंटी खड़कने लगी....अनायस सिर शीशे से ऊपर उठ गया। आतुर प्रतीक्षा में फैली मेरी आँखे बन्द दरवाज़े पर टिक गई। घंटी बजती रही....वह हॉस्टल का कॉमन टेलीफोन था, दस कमरों के कॉरीडोर के बीचोंबीच। पुरानी आदत मुझे दरवाजे के पास घसीट लाई थी। मैं कान लगाए सुन रहा था। मुझमें इतना साहस भी नहीं होता था कि स्वयं बाहर आकर रिसीवर उठा लूँ। घंटी की चीखती आवाज़ मेरी चेतना की परत को महज छू आती थी....आगे कुछ भी नहीं था। यह मैं जानता था, फिर भी मैं धीरे-धीरे काँपने लगा था। एक भयंकर थपाटे से किसी कमरे का दरवाजा़ खुला था। कॉरीडोर के पुराने फर्श पर जूतों की आवाज़....टेलीफ़ोन की ओर तेज़ी से बढ़ती हुई।
क्या यह उसका नाम है ? पहले हमेशा यही होता था.....शाम की इस घड़ी में। मैं जूते-मोज़े पहनकर बिस्तर पर लेटा रहा करता था। दोपहर से शाम की इस घड़ी की प्रतीक्षा में......टेलीफोन की घँटी बजती थी.....जूतों की आवाज़ मेरे दरवाज़े के सामने ठहर जाती थी......
रूम नम्बर 13 टेलीफ़ोन !
मैंने झपटकर दरवाजे़ का हैंडिल पकड़ लिया। दिसम्बर के इस मौसम में भी मेरी हथेलियाँ पसीने से तर थीं। किसी ने मेरा दरवाज़ा नहीं खटखटाया.....जूतों की आवाज़ मेरे दरवाज़े के निकट आई......लेकिन रुकी नहीं, केवल मेरी साँस को रोककर आगे बढ़ गई। मैं मुड़ा, और दरवाज़े से पीठ सटाकर कमरे की ओर देखने लगा।
मुझे आश्चर्य हुआ। सब-कुछ वैसा ही था-बेसिन के आले में रखा साबुन, साबुन में लिथड़ा ब्रुश, टप-टप नल की बूँदें। बाहर कॉरीडोर में अब सम्पूर्ण शान्ति थी.....सिर्फ़ हवा चलने से रोशनदान में फँसा अखबार फड़फड़ाने लगता था।
मैं दबे कदमों से आगे बढ़ा, जैसे चोरी-चुपके से किसी पराए कमरे में चले आया हूँ। अपने बिस्तर के पास आकर मेरे पाँव ठिठक गए। मैं काँपते हाथों से सिरहाने की दीवार छूने लगा......दीवार से सिर्फ उस हिस्से को, जो पीठ की रगड़ से स्याह पड़ गया था। एक लम्बी-पतली पीठ का निशान..........
‘‘सुनो !’’ अँधेरे में किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया है। मेरी काँपती अँगुलियाँ दीवार पर टिकी रहती हैं....सच बताओ....क्या तुम बिल्कुल विश्वास नहीं करते ?
यह आवाज़ उसकी है। कितनी बार उसने उसे सुना है।
लगता है, उसके चले जाने के बाद भी यह आवाज़ पीछे छूट गई थी-अपने में अलग और सम्पूर्ण। मैं खिड़की खोलता हुआ डरता हूँ......दरवाज़े पर भी कोई दस्तक देता है, तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है......लगता है, ज़रा-सा भी रास्ता पाने पर यह आवाज़ बाहर निकल जाएगी और मुझे पकड़ लेगी। मैं कब तक उसे रोक सकूँगा-अधीर-आग्रहपूर्ण, आँसुओं में भीगी उस आवाज़ को, जैसा मैंने उसे रात की अकेली घड़ी में सुना था ?
मैं देर तक कमरे की अँगीठी के सामने खड़ा रहा। सर्दी बढ़ गई थी और मैं गर्म ऊनी जैकेट के भीतर भी ठिठुर रहा था। फिर भी मैं आग जलाने की हिम्मत नहीं बटोर सका। कुहरे में ढँकी खिड़की के पीछे डाइनिंग-हॉल की बत्ती जली थी....बर्फ़ के छोटे-छोटे गाले सफ़ेद तितलियों से रोशनी को छूते हुए अँधेरे में गायब हो जाते थे।
सफ़ेद, खामोश बर्फ़।
किसी ने धीमे से दरवाज़ा खटखटाया था....मैं सो रहा था और एकदम चौंककर उठ गया। आँखें दरवाज़े पर टिक गईं।
-रूम नंबर 13...यू हैव टेलीफ़ोन ! सोते हुए मैं घंटी नहीं सुन सका था। चप्पल पहनकर कॉरीडोर में आया......इस समय मुझे कौन बुला सकता है ? क्रिसमस की छुट्टियाँ आरम्भ हो चुकी थीं और मेरे लगभग सभी मित्र प्राग से बाहर चले गए थे। मैंने रिसीवर उठाया.......एक भारी, अपरिचित स्वर सुनाई दिया, ‘‘क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं......हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।’’
‘‘अभी ?’’ मैंने हाथ पर लगी घड़ी देखी.....आठ से अधिक समय नहीं हुआ था.....मैं शाम को अचानक सो गया था और नींद अब भी मेरी अलसाई नसों पर रेंग रही थी। ‘‘क्या कल आना नहीं हो सकेगा ?’’ मैंने झिझकते हुए कहा। ‘‘कल..?’’ रिसीवर में एक क्षण तक सन्नाटा रहा...फिर वही आवाज़ सुनाई दी...इस बार बौखलाई-सी, ‘‘ईश्वर के लिए....अभी। हो सके तो टैक्सी लेकर आ जाइए....क्या आपको पता मालूम है ?’’
एक क्षण के लिए जी में आया कि मैं जाने से इनकार कर दूँ।
‘टूरिस्ट एजेन्सी’ को इस समय मुझसे क्या काम हो सकता है, मैं कोई अनुमान नहीं लगा सका।
‘‘मुझे आधा घंटा लग जाएगा।’’ मैंने कहा।
‘‘ओ के, ठीक है....हम प्रतीक्षा कर रहे हैं....हो सके तो टैक्सी ले लीजिए.....वी शैल पे फॉर इट...’’
मैंने रिसीवर रख दिया। टेलीफ़ोन के पास ही होस्टल का प्राइवेट किचन था। कुछ अरब विद्यार्थी वहाँ खड़े थे....माकरोनी और तली हुई मछली की गन्ध कॉरीडोर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल रही थी। ब्लॉक के कोने में सीढ़ियों के पास, एक नीग्रो छात्र किसी चेक लड़की से बहुत धीमे दबे स्वर में बातचीत कर रहा था। यह पुराने हास्टल की पुरानी मंज़िल थी.....यहाँ सिर्फ़ फ़ाइन-आर्ट्स के विद्यार्थी रहते थे। शाम के समय अक्सर कमरों में वायलन या सेक्सोफोन की आवाज़े सुनाई देती थीं। लेकिन छुट्टियों में होस्टल उजाड़ हो जाता.......सिवाय कुछ विदेशी छात्र आख़िर तक बने रहते।
मैं अपने कमरे में आया और फ्राइंग-पैन को स्टोव पर रख दिया। अलमारी के निचले दराज़ से प्याज़, मार्जरीन और मछली का टिन बाहर निकाला। बाउन-ब्रेड की दो कतरी हुई स्लाइसें मेज़ पर रख दी......मैं सोता रहा था और अब मुझे अचानक भूख लग आई थी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i