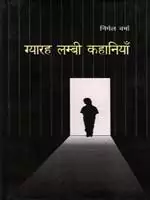|
लेख-निबंध >> कला का जोखिम कला का जोखिमनिर्मल वर्मा
|
82 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है वैयक्तिक निबंध...
kala ka jokhim
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
निर्मल वर्मा के निबन्ध-संग्रहों के सिलसिले में कला का जोखिम उनकी दूसरी पुस्तक है, जिसका पहला संस्करण लगभग बीस साल पहले आया था। स्वंय निर्मल जी द्वारा इस पुस्तक को अपने पहले निबन्ध-संग्रह शब्द और स्मृति तथा बाद वाले ढलान से उतरते हुए शीर्षक संग्रह के बीच की कड़ी मानते हैं जो इन दोनों पुस्तकों में व्यक्त चिन्ताओं को आपस में जोड़ती है।
निर्मल वर्मा के चिन्तक का मूल सरोकार ‘आधुनिक सभ्यता में कला के स्थान’ को लेकर रहा है। मूल्यों के स्तर पर कला, सभ्यता के यांत्रिक विकास में मनुष्य को साबुत, सजीव और संघर्षशील बनाए रखने वाली भावात्मक उर्जा है, किन्तु इस युग का विशिष्ट अभिशाप यह है कि जहाँ कला एक तरफ मनुष्य के कार्य-कलाप से विलगित हो गयी, वहाँ दूसरी तरफ वह एक स्वायत्त सत्ता भी नहीं बन सकी है, जो स्वयं मनुष्य की खंडित अवस्था को अपनी स्वतंत्र गरिमा से अनुप्राणित कर सके।’
साहित्य और विविध देश-कालगत सन्दर्भों से जुड़े ये निबन्ध लेखक की इसी मूल पीड़ा से हमें अवगत कराते हैं। अपनी ही फेंकी हुई कमन्दों में जकड़ी जा रही सभ्यता में कला की स्वायत्तता का प्रश्न ही कला का जोखिम है और साथ ही ज्यादा महत्त्वपूर्ण यह है कि ‘वही आज रचनात्मक क्रान्ति की मूल चिन्ता का विषय’ बन गया है। इन निबन्धों के रूप में इस चिन्ता से जुड़ने का अर्थ एक विधेय सोच से जुड़ना है और कला का ज्यादा स्वाधीन इकाई के रूप में प्रतिष्ठित हो सके, उसके लिए पर्याप्त ताकत जुटाना भी।
निर्मल वर्मा के चिन्तक का मूल सरोकार ‘आधुनिक सभ्यता में कला के स्थान’ को लेकर रहा है। मूल्यों के स्तर पर कला, सभ्यता के यांत्रिक विकास में मनुष्य को साबुत, सजीव और संघर्षशील बनाए रखने वाली भावात्मक उर्जा है, किन्तु इस युग का विशिष्ट अभिशाप यह है कि जहाँ कला एक तरफ मनुष्य के कार्य-कलाप से विलगित हो गयी, वहाँ दूसरी तरफ वह एक स्वायत्त सत्ता भी नहीं बन सकी है, जो स्वयं मनुष्य की खंडित अवस्था को अपनी स्वतंत्र गरिमा से अनुप्राणित कर सके।’
साहित्य और विविध देश-कालगत सन्दर्भों से जुड़े ये निबन्ध लेखक की इसी मूल पीड़ा से हमें अवगत कराते हैं। अपनी ही फेंकी हुई कमन्दों में जकड़ी जा रही सभ्यता में कला की स्वायत्तता का प्रश्न ही कला का जोखिम है और साथ ही ज्यादा महत्त्वपूर्ण यह है कि ‘वही आज रचनात्मक क्रान्ति की मूल चिन्ता का विषय’ बन गया है। इन निबन्धों के रूप में इस चिन्ता से जुड़ने का अर्थ एक विधेय सोच से जुड़ना है और कला का ज्यादा स्वाधीन इकाई के रूप में प्रतिष्ठित हो सके, उसके लिए पर्याप्त ताकत जुटाना भी।
नए संस्करण के बारे में
‘कला का जोखिम’ मेरे निबन्ध-संग्रह की दूसरी पुस्तक है, जो ‘शब्द और स्मृति’ (1976) के बाद प्रकाशित हुई थी। लगभग बीस वर्ष बाद इसका नया संस्करण प्रकाशित करते हुए प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। दरअसल यह पुस्तक एक तरह से बीच की कड़ी है, ‘शब्द और स्मृति’ तथा ‘ढलान से उतरते हुए’ को परस्पर जोड़ती हुई। आशा करता हूँ कभी भविष्य में ये तीनों एक जिल्द में प्रकाशित हो सकेंगी, ताकि पाठक उन्हें एक साथ पढ़ सकें।
नये संस्करण में मैंने केवल भाषा के कुछ संशोधन किए हैं, विशेषकर उन लेखों में, जिनका अनुवाद अंग्रेजी से किया गया था। अपनी कुछ मान्यताओं को आज इतने बरसों बाद मैं कुछ अन्य रूप में प्रस्तुत कर सकता था किन्तु उनमें सन्निहित विश्वास सही हैं जिनसे उत्प्रेरित होकर मैंने ये निबन्ध लिखे थे। अतः मैंने उनमें अधिक छेड़छाड़ नहीं की है। वे मेरी चिन्तन यात्रा के एक महत्त्वपूर्ण मोड़ को इंगित करते हैं जिनमें मैंने किसी तरह का परिवर्तन करना उचित नहीं समझा।
इस अवसर पर मैं अपने पाठकों के प्रति कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे निबन्धों को मेरी कहानियों से अलग नहीं बल्कि उनका पूरक माना है। उनके सतत उत्साह और सहृदयता ने ही मुझे-अक्सर आलोचना की मुख्यधारा के विरुद्ध बराबर लिखते रहने के लिए प्रेरित किया है।
यह संस्करण उन्हीं के हाथों सौंपते हुए मैं अपना आभार प्रगट करना चाहूँगा।
नये संस्करण में मैंने केवल भाषा के कुछ संशोधन किए हैं, विशेषकर उन लेखों में, जिनका अनुवाद अंग्रेजी से किया गया था। अपनी कुछ मान्यताओं को आज इतने बरसों बाद मैं कुछ अन्य रूप में प्रस्तुत कर सकता था किन्तु उनमें सन्निहित विश्वास सही हैं जिनसे उत्प्रेरित होकर मैंने ये निबन्ध लिखे थे। अतः मैंने उनमें अधिक छेड़छाड़ नहीं की है। वे मेरी चिन्तन यात्रा के एक महत्त्वपूर्ण मोड़ को इंगित करते हैं जिनमें मैंने किसी तरह का परिवर्तन करना उचित नहीं समझा।
इस अवसर पर मैं अपने पाठकों के प्रति कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे निबन्धों को मेरी कहानियों से अलग नहीं बल्कि उनका पूरक माना है। उनके सतत उत्साह और सहृदयता ने ही मुझे-अक्सर आलोचना की मुख्यधारा के विरुद्ध बराबर लिखते रहने के लिए प्रेरित किया है।
यह संस्करण उन्हीं के हाथों सौंपते हुए मैं अपना आभार प्रगट करना चाहूँगा।
6 जून, 2001
भूमिका
पुस्तक में अधिकांश वही लेख और निबन्ध शामिल किए गए हैं, जिन्हें मैंने पिछले ढाई-तीन वर्षों के दौरान लिखा था-अथवा विशेष मौकों पर गोष्ठियों या सेमीनारों में पढ़ा था। किन्तु एक दो लेख ऐसे भी हैं, जिनका रचनाकाल काफी पुराना है; उदाहरणत: संग्रह का पहला निबन्ध ‘कला, मिथक और यथार्थ’ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला, (1974) में मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसका हिन्दी अनुवाद पहली बार इस पुस्तक में जा रहा है। ‘रचना की जरूरत’ त्रिनाले के अन्तर्गत आयोजित अन्तर्राष्टीय विचार गोष्ठी में अंग्रेजी में पढ़ा गया था, जिसका हिन्दी अनुवाद श्री शानी ने किया है। संग्रह का अन्तिम निबन्ध ‘सुलगती टहनी’-जो निबन्ध से अधिक एक यात्रा-चिन्तन है-मेरी विविध रचनाओं के संकलन (दूसरी दुनिया) से लिया गया है, क्योंकि मेरे विचार में इसका सही और उचित स्थान अपने समकालीन निबन्धों के साथ ही है।
आप जैसा देखेंगे, पुस्तक में संग्रहीत ये निबन्ध किसी-न-किसी कोने से बराबर एक केन्द्रीय बिन्दु को छूने का प्रयास करते हैं-और वह है, आधुनिक सभ्यता में कला का स्थान। पिछले वर्षों मुझे लगता रहा है कि हमारी दुनिया में कला का स्थान दिनोदिन धुँधला, अनिश्चित और सन्दिग्ध बनता गया है, जो मेरी समझ में कला का सबसे बीहड़ जोखिम है। बीसवीं शती के आरम्भ में ‘आधुनिक कला’ ने जिस औद्योगिक सभ्यता की चुनौती में-और उसके बीच अपनी शक्तियों को समेटा था, आज इस शती की ढलती घड़ियों में-आधुनिक सभ्यता ने मानो प्रतिशोध में स्वयं कला को मनुष्य के जीवन में सन्देहास्पद बना दिया है। यदि केवल ‘सन्देह’ की स्थिति होती, तो शायद बहुत चिन्ता की बात न होती-हर युग में कला कमोबेश सन्दिग्ध रही है, दुनिया की आँखों में-किन्तु हमारे युग का विशिष्ट अभिशाप यह है कि जहाँ कला एक तरफ मनुष्य के कार्य का विशिष्ट अभिशाप यह है कि जहाँ कला एक तरफ मनुष्य के कार्य कलाप से विलगित हो गई है,वहाँ दूसरी तरफ वह एक स्वायत्त सत्ता भी नहीं बन सकी है, जो स्वयं मनुष्य की खंडित अवस्था को अपनी स्वतन्त्र गरिमा से अनुप्राणित कर सके। कला का जोखिम शायद यही है कि क्या वह आज की जड़ित, पराधीन होती हुई सभ्यता में सम्पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रह सकेगी-और स्वतन्त्र रहकर भी अपने अलगाव का अतिक्रमण कर सकेगी ?
यह संयोग नहीं है और बहुत महत्त्वपूर्ण है कि जो कला का जोखिम है, वही आज रचनात्मक क्रान्ति की मूल चिन्ता का विषय भी बन गए है। आधुनिक समाज में क्या मनुष्य स्वतन्त्र रहकर भी अपने अधूरेपन के अभिशाप से छुटकारा पा सकता है ? मैं समझता हूँ, हमारे समय में जय प्रकाश जी ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने इसका उत्तर अपने चिन्तन और जीवन कर्म में दिया था। वह कलाकार नहीं थे, किन्तु उनकी जिन्दगी एक ऐसी सम्पूर्ण रचना थी, जो स्वयं कला को उपकृत करती थी। पुस्तक के ‘रचनाकार खंड’ में जहाँ रेणु हैं, वहाँ जयप्रकाशजी भी हैं।
यह पुस्तक उन दोनों की स्मृति को समर्पित है।
आप जैसा देखेंगे, पुस्तक में संग्रहीत ये निबन्ध किसी-न-किसी कोने से बराबर एक केन्द्रीय बिन्दु को छूने का प्रयास करते हैं-और वह है, आधुनिक सभ्यता में कला का स्थान। पिछले वर्षों मुझे लगता रहा है कि हमारी दुनिया में कला का स्थान दिनोदिन धुँधला, अनिश्चित और सन्दिग्ध बनता गया है, जो मेरी समझ में कला का सबसे बीहड़ जोखिम है। बीसवीं शती के आरम्भ में ‘आधुनिक कला’ ने जिस औद्योगिक सभ्यता की चुनौती में-और उसके बीच अपनी शक्तियों को समेटा था, आज इस शती की ढलती घड़ियों में-आधुनिक सभ्यता ने मानो प्रतिशोध में स्वयं कला को मनुष्य के जीवन में सन्देहास्पद बना दिया है। यदि केवल ‘सन्देह’ की स्थिति होती, तो शायद बहुत चिन्ता की बात न होती-हर युग में कला कमोबेश सन्दिग्ध रही है, दुनिया की आँखों में-किन्तु हमारे युग का विशिष्ट अभिशाप यह है कि जहाँ कला एक तरफ मनुष्य के कार्य का विशिष्ट अभिशाप यह है कि जहाँ कला एक तरफ मनुष्य के कार्य कलाप से विलगित हो गई है,वहाँ दूसरी तरफ वह एक स्वायत्त सत्ता भी नहीं बन सकी है, जो स्वयं मनुष्य की खंडित अवस्था को अपनी स्वतन्त्र गरिमा से अनुप्राणित कर सके। कला का जोखिम शायद यही है कि क्या वह आज की जड़ित, पराधीन होती हुई सभ्यता में सम्पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रह सकेगी-और स्वतन्त्र रहकर भी अपने अलगाव का अतिक्रमण कर सकेगी ?
यह संयोग नहीं है और बहुत महत्त्वपूर्ण है कि जो कला का जोखिम है, वही आज रचनात्मक क्रान्ति की मूल चिन्ता का विषय भी बन गए है। आधुनिक समाज में क्या मनुष्य स्वतन्त्र रहकर भी अपने अधूरेपन के अभिशाप से छुटकारा पा सकता है ? मैं समझता हूँ, हमारे समय में जय प्रकाश जी ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने इसका उत्तर अपने चिन्तन और जीवन कर्म में दिया था। वह कलाकार नहीं थे, किन्तु उनकी जिन्दगी एक ऐसी सम्पूर्ण रचना थी, जो स्वयं कला को उपकृत करती थी। पुस्तक के ‘रचनाकार खंड’ में जहाँ रेणु हैं, वहाँ जयप्रकाशजी भी हैं।
यह पुस्तक उन दोनों की स्मृति को समर्पित है।
नयी दिल्ली
14 फरवरी 1981
14 फरवरी 1981
निर्मल वर्मा
कला, मिथक और यथार्थ
we are our own demons, we expel ourselves from our paradise.
ग्रोयटे
मनुष्य का आत्मबोध-यह कि मैं हूँ और मनुष्य हूँ-इतिहास में कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। हम इस घटना, इस आत्मबोध के इतने आदी हो गए हैं कि लगता है मानो यह मानव स्वभाव का कोई शाश्वत तत्त्व हो उसके मनुष्य तत्त्व से जुड़ा हुआ, मनुष्य की चेतना का अभिन्न भाव चिरन्तन और सार्वभौम-जिसका दिशा काल से कोई सन्बन्ध न हो। हम अक्सर भूल जाते हैं कि मनुष्य की आत्मचेतना-कि मैं धरती पर अकेला अजनबी हूँ और स्वयं अपनी नियति के लिए जवाबदेह हूँ-यहूदी-ईसाई परम्परा का अंग है जिसने पश्चिमी सभ्यता को एक विशिष्ट आध्यात्मिक चरित्र प्रदान किया था। इस परम्परा की अन्तिम परिणति-तार्किक परिणति-रेनेसेंस मनुष्य के उस सर्वांगीण व्यक्तित्व में प्रस्फुटित हुई, जिसे अपने ‘अहं’ पर भरोसा था, जो धरती के केन्द्र में था, (उसी तरह जैसे धरती सौरमंडल के केन्द्र में थी), जिसकी कसौटी पर दुनिया की हर चीज नापी जाती थी-आत्मविश्वासी, आत्मकेन्द्रित, गर्वीला मनुष्य।
मनुष्य को अपने इस गरिमा-मंडित आत्मगौरव के लिए काफी भारी मूल्य चुकाना पड़ा। मध्यकाल में वह अपने विश्वासों के भीतर सुरक्षित था-चर्च की चहारदीवारी के भीतर इन विश्वासों पर शंका या सन्देह की आँच नहीं आ सकती थी। सुरक्षा की यह गरमाई आज भी हम यूरोप की मॉनेस्टरियों में देख सकते हैं, जिनकी तंग सँकरी कोठरियों में भिक्षुक और भिक्षुणियाँ अपना जीवन बिताते थे। एक बन्द समाज में मनुष्य स्वतन्त्र न भी हो, अपेक्षाकृत सुरक्षित रह सकता है, इसकी कल्पना कम-से-कम भारतवासी कर सकते हैं-या कुछ दशक पहले तक कर सकते थे। किन्तु यूरोप में रेनेसेंस के बाद सुरक्षा की ये दीवारें एक-एक करके ढहने लगीं। मनुष्य अब खुले में था। स्वाधीन किन्तु अरक्षित। एक समय में ईसाई विश्वदर्शन ने मनुष्य और दुनिया के बीच जो सेतु बनाया था, वह सहसा डगमगाने लगा था।
लूथर ने जो आघात चर्च की आस्था पर किया था, वह कुछ इतना गहरा था कि उसकी भग्न दरारों के बीच पहली बार आत्मशंका की छाया ने निकलकर यूरोपीय मानस को विचलित और उद्वेलित कर दिया था। अब मनुष्य अपने से भागकर कहीं और सिर नहीं छिपा सकता था। पास्कल शायद पहले ईसाई चिन्तक, थे जिन्होंने यूरोपीय मनुष्य के उस भयावह आतंक को समझा था, जो ब्रह्मांड के सूने मौन से उत्पन्न होता है। पहली बार मनुष्य के भीतर यदि ‘चिन्ता’ (anxiety) की अनुभूति हुई, तो शायद इस बिन्दु पर जब धर्मचेतना के धुँधले हाशिये पर लुप्त होता गया और दूसरी तरफ मनुष्य का अपना ‘मैं’, अपनी गौरवपूर्ण अस्मिता एक ऐसे संकीर्ण, अहंग्रस्तदायरे में सिकुड़ गई, जहाँ वह अपने भीतर के अँधेरे के समक्ष नितान्त अवश पड़ता गया। क्या मतलब है इस अँधेरे का ? इस प्रश्न के सामने वह बिल्कुल निरुत्तर था। अब मनुष्य विश्व के केन्द्र में नहीं, अपने शून्य के केन्द्र में था-और वहाँ वह बिल्कुल अकेला था।
इसलिए मनुष्य का आत्मबोध अपने होने की चेतना मानव स्वभाव का कोई शाश्वत गुण नहीं है; वह एक प्रक्रिया है जो इतिहास में घटती है-एक दुर्घटना और वरदान दोनों ही। इस प्रक्रिया में आशा और अपशगुन दोनों ही निहिति हैं-स्वतन्त्रता की आशा और अकेलेपन का अपशगुन। मनुष्य की आत्मचेतना दार्शनिक अर्थ में नहीं, जहाँ वह आत्मज्ञान होती है-बल्कि जैविक विकास के अर्थ में-जहाँ मनुष्य को अपने होने, अपने अस्तित्व का बोध होता है-वह आत्मचेतना व्यक्ति की मानसिकता में एक फाँक खींच देती है-और यह फाँक, यह दरार उतनी ही गहरी और विध्वंसात्मक है, जितना वह प्राथमिक पतन जब मानव जाति पहली बार प्रकृति के अभिन्न सम्बन्ध से टूटी थी, विलगित हुई थी और उसने एक सर्वथा उदासीन, सर्वथा भावशून्य विश्व में अपने को नितान्त सीमित, क्षुद्र और क्षणभंगुर पाया था। आज की सभ्यता का संकट और प्रदूषण उस ऐतिहासिक क्षण से शुरू हो गया था, जब मनुष्य प्रकृति से अलग छिटक गया था यह मानव-सभ्यता और मनुष्य की यातना का समान स्रोत है, जो आज हमें घसीटकर ‘अणु युग’ तक ले आया है।
मनुष्य का यह दुहरा अलगाव-प्रकृति से विलगित होना और समाज से अलग टूट जाना-यद्यपि ऐतिहासिक प्रक्रिया के दो अलग-अलग क्षण हैं, किन्तु मनुष्य की चेतना पर उनका प्रभाव बहुत कुछ एक जैसा है-दोनों स्थितियों में ही मनुष्य के भीतर एक भयावह अकेलापन अनाथ हो जाने की कातरता उत्पन्न हो जाती है, वास्तव में जब हम किसी ‘समग्र इकाई’ से टूटते हैं (चाहे वह बच्चे का माँ के गर्भ से अलग होना ही क्यों न हो) तो यह अनाथ-भाव अनिवार्य रूप से हमें आक्रान्त करता है। किन्तु प्रकृति से अलगाव कहीं बहुत गहरे में समाज के अलगाव से भिन्न है; प्रागैतिहासिक-काल का आदिवासी प्रकृति से अलग टूटकर कम-से-कम अपने समूह से जुड़ा रहता है जिसके परिणामस्वरूप उसके निजी अनुभव एक वृहत्तर अनुभव, एक सामूहिक चेतना का ही अंश हैं, जिसमें वह दूसरों के अनुभवों में साझा करता है और दूसरे उसके अनुभव में भाग लेते हैं। किन्तु इससे भिन्न एक सभ्य मनुष्य की आत्मचेतना केवल अपने तक ही केन्द्रित रहती है-उसका निजी व्यक्तित्व एक सम्पूर्ण इकाई है, जिसके भीतर वह समूची बाहरी दुनिया को समेट लेता है-जिसके कारण वह अपने को दूसरों के साथ नहीं, दूसरों के समक्ष या विरुद्ध पाता है। उसका अनुभव यदि दूसरों के अनुभवों में साझा भी करता है, तो अपनी शर्तों पर, एक विराट अनुभव का अंश बनकर नहीं, और जब वह अपने को किसी वृहत्तर इकाई (राज्य तानाशाह या जाति) के प्रति समर्पित करता हूँ, तो भी यह भावना कि ‘मैं अपने को विलय कर रहा हूँ’, उसकी चेतना पर एक याद, एक खरोंच की तरह दगी रहती है।
ऐतिहासिक सभ्य मनुष्य की यह पीड़ा कि वह दूसरों से भिन्न या उनके विरुद्ध है-उस प्रागैतिहासिक मनुष्य की पीड़ा से भिन्न या उनके विरुद्ध है-उस प्रागैतिहासिक मनुष्य की पीड़ा से एक गहरे अर्थ में अलग हो जाती है, जो अपने को प्रकृति के समक्ष तो अकेला पाता है, किन्तु अपने भीतर अकेला महसूस नहीं करता। वास्तव में मिथकों का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वे प्रागैतिहासिक मनुष्य के उस आघात और आतंक को कम कर सकें, जो उसे प्रकृति से सहसा अलग होने पर महसूस हुआ था-और मिथक यह काम केवल एक तरह से ही कर सकते थे-स्वयं प्रकृति और देवताओं का मानवीकरण करके। इस अर्थ में मिथक एक ही समय में मनुष्य के अलगाव को प्रतिबिम्बित करते हैं, और उस अलगाव से जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उससे मुक्ति भी दिलाते हैं। प्रकृति से अभिन्न होने का नॉस्टाल्जिया, प्राथमिक स्मृति की कौंध, शाश्वत और चिरन्तन से पुनः जुड़ने का स्वप्न ये भावनाएँ मिथक को सम्भव बनाने में सबसे सशक्त भूमिका अदा करती हैं। सच पूछें, तो मिथक और कुछ नहीं प्रागैतिहासिक मनुष्य का एक सामूहिक स्वप्न है जो व्यक्ति के स्वप्न की तरह काफी अस्पष्ट, संगतिहीन और संश्लिष्ट भी है। कालान्तर में पुरातन अतीत की ये अस्पष्ट गूँजें, ये धुँधली आकांक्षाएँ एक तर्कसंगत प्रतीकात्मक ढाँचे में ढल जाती हैं और प्राथमिक यथार्थ की पहली, क्षणभंगुर, फिसलती यादें महाकाव्यों (epik) की सुनिश्चित संरचना में गठित होती हैं। मिथक और इतिहास के बीच महाकाव्य एक सेतु है, जो पुरातन स्वप्नों को काव्यात्मक ढाँचे में अवतरित करता है।
किन्तु महाकाव्य के बुनियादी ‘पैटर्न’ और रूप-गठन का आधार अब भी बहुत हद तक वही ‘मिथक-दृष्टि’ है, जिसके सहारे आदि मनुष्य यथार्थ का बोध प्राप्त करता था, बाहरी दुनिया से अपना रिश्ता जोड़ता था। एक-दूसरे से जुड़े तथ्य और घटनाएँ महाकाव्य के लेखक आदि कवि को उतना प्रभावित नहीं करतीं, जितना सामूहिक अवचेतना से जुड़े रूपक (metaphor) उसकी अन्तर्चेतना को अनुप्राणित और आलोकित करते हैं। रूपक से तथ्य और मिथक से तर्क की तरफ बढ़ती हुई मनुष्य की मानसिकता एक तरह से उस ऐतिहासिक विकास (यदि हम उसे ‘विकास’ कह सकें) को ही रेखांकित करती है, जब मनुष्य की सामूहिक अवचेतना धीरे-धीरे व्यक्ति की आत्मचेतना में परिणत होने लगी थी।
महाकाव्य के मिथकीय नायक का अपनी नियति से सम्बन्ध उतना ही समग्र और सहज है, जितना आदिमनुष्य का सम्बन्ध अन्य व्यक्ति से था; वह सामंजस्य और स्वीकृति का रिश्ता है-विरोध और प्रतिरोध का नहीं। इस रिश्ते में एक तरह का अनिवार्यता है, जो उसे निर्मम और कठोर तो बनाती है, लेकिन त्रासद कभी नहीं। ईलियड में आर्खलीस और महाभारत में कर्ण की नियति जीवनधारा का आत्मसमर्पित (आत्मसंकल्पित नहीं) अंग है, जो उसे देवताओं द्वारा रचित वृहत्तर नाटक से जोड़ देती है। मृत्यु का क्षण त्रासद नहीं होता, क्योंकि वह सम्पूर्ण उपलब्धि का क्षण भी है। किन्तु यह बात हैमलेट पर लागू नहीं होती। वह अपने पिता की हत्या के तथ्य के सामने बिल्कुल अकेला है-और यह तथ्य किसी क्रम, किसी पैटर्न, देवताओं के किसी नाटक में फिट नहीं होता-कभी वह हत्या एक घुन की तरह हैमलेट की आत्मा को खाए जाती है। आर्खलीस के जीवन में उसकी मृत्यु एक अनिवार्य परिणति है, जबकि हैमलेट जिन्दगी के साथ झगड़ता हुआ खत्म हो जाता है-बीच बहस में। होमर से शेक्सपियर तक आते-आते मनुष्य की चेतना में आधारभूत परिवर्तन हो चला था-जहाँ पहले वह अपनी प्रकृति नियति से सम्पूर्ण रूप से जुड़ा था, वहाँ कालान्तर में उसकी आत्मा और नियति के बीच एक काली दरार खिंचती गई और यह दरार इतनी गहरी थी कि वह स्वयं अपनी प्रकृति से निर्वासित होता गया। कला में यह परिवर्तन सीधा सृजन-प्रक्रिया में हुआ; पहले कला जहाँ एक अचेतन रचना थी, अब यह रचनात्मक चेतना की अभिव्यक्ति बन गई; किर्केगार्द जिसे ‘सम्पूर्ण सम्भावना’ कहते थे अब वह टूटकर सन्दिग्ध विकल्पों में बँट गई, जिसमें से कोई भी विकल्प मनुष्य चुन सकता था, किन्तु इस चयन का कोई विश्वसनीय दैवी या नैतिक अनुसमर्थन कहीं न था।
यह वह क्षण था, जब मनुष्य का पहली बार अपने ‘मैं’ इगो से साक्षात्कार हुआ, एक ऐसी आत्मभ्रमित चीज जो स्वयं अपने भीतर खंडित थी। पहले जहाँ मनुष्य अपने भीतर समूची वास्तविकता लेकर चलता था, अब वहाँ सिर्फ खोई हुई दुनिया की एक अपाहिज पंगु स्मृति शेष रह गई थी, वह दुनिया खो गई थी, लेकिन मनुष्य उसे भूल नहीं सका था। वास्तव में ‘ईश्वर की मृत्यु’ को लेकर नीत्शे के भयानक आर्तनाद की पीछे यह कातर आकांक्षा छिपी थी कि उस शब्द को दुबारा खोजा जा सके, जो मनुष्य और मिथक को जोड़ता था। एक ऐसे जीवन्त अनुभव का प्रतीक जिसे मनुष्य के अहम बोध ने इतनी बुरी तरह आहत कर दिया था। यह मनुष्य का पतन था। सच कहें, तो दूसरा पतन क्योंकि पहला पतन वह था, जब वह प्रकृति से खंडित हुआ था। मिथक, जो एक समय में मनुष्य के सर्वांगीण, सम्पूर्ण व्यक्तित्व का पोषक था, अब आत्मपीड़ित स्मृतियों के जाले में बदल गया, मनुष्य के खंडित, ज्वरग्रस्त स्वप्नों में उलझा हुआ, जिसे सिर्फ फ्रायड की सूक्तियों और सिद्धान्तों में ही पकड़ा जा सकता था।
ग्रोयटे
मनुष्य का आत्मबोध-यह कि मैं हूँ और मनुष्य हूँ-इतिहास में कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। हम इस घटना, इस आत्मबोध के इतने आदी हो गए हैं कि लगता है मानो यह मानव स्वभाव का कोई शाश्वत तत्त्व हो उसके मनुष्य तत्त्व से जुड़ा हुआ, मनुष्य की चेतना का अभिन्न भाव चिरन्तन और सार्वभौम-जिसका दिशा काल से कोई सन्बन्ध न हो। हम अक्सर भूल जाते हैं कि मनुष्य की आत्मचेतना-कि मैं धरती पर अकेला अजनबी हूँ और स्वयं अपनी नियति के लिए जवाबदेह हूँ-यहूदी-ईसाई परम्परा का अंग है जिसने पश्चिमी सभ्यता को एक विशिष्ट आध्यात्मिक चरित्र प्रदान किया था। इस परम्परा की अन्तिम परिणति-तार्किक परिणति-रेनेसेंस मनुष्य के उस सर्वांगीण व्यक्तित्व में प्रस्फुटित हुई, जिसे अपने ‘अहं’ पर भरोसा था, जो धरती के केन्द्र में था, (उसी तरह जैसे धरती सौरमंडल के केन्द्र में थी), जिसकी कसौटी पर दुनिया की हर चीज नापी जाती थी-आत्मविश्वासी, आत्मकेन्द्रित, गर्वीला मनुष्य।
मनुष्य को अपने इस गरिमा-मंडित आत्मगौरव के लिए काफी भारी मूल्य चुकाना पड़ा। मध्यकाल में वह अपने विश्वासों के भीतर सुरक्षित था-चर्च की चहारदीवारी के भीतर इन विश्वासों पर शंका या सन्देह की आँच नहीं आ सकती थी। सुरक्षा की यह गरमाई आज भी हम यूरोप की मॉनेस्टरियों में देख सकते हैं, जिनकी तंग सँकरी कोठरियों में भिक्षुक और भिक्षुणियाँ अपना जीवन बिताते थे। एक बन्द समाज में मनुष्य स्वतन्त्र न भी हो, अपेक्षाकृत सुरक्षित रह सकता है, इसकी कल्पना कम-से-कम भारतवासी कर सकते हैं-या कुछ दशक पहले तक कर सकते थे। किन्तु यूरोप में रेनेसेंस के बाद सुरक्षा की ये दीवारें एक-एक करके ढहने लगीं। मनुष्य अब खुले में था। स्वाधीन किन्तु अरक्षित। एक समय में ईसाई विश्वदर्शन ने मनुष्य और दुनिया के बीच जो सेतु बनाया था, वह सहसा डगमगाने लगा था।
लूथर ने जो आघात चर्च की आस्था पर किया था, वह कुछ इतना गहरा था कि उसकी भग्न दरारों के बीच पहली बार आत्मशंका की छाया ने निकलकर यूरोपीय मानस को विचलित और उद्वेलित कर दिया था। अब मनुष्य अपने से भागकर कहीं और सिर नहीं छिपा सकता था। पास्कल शायद पहले ईसाई चिन्तक, थे जिन्होंने यूरोपीय मनुष्य के उस भयावह आतंक को समझा था, जो ब्रह्मांड के सूने मौन से उत्पन्न होता है। पहली बार मनुष्य के भीतर यदि ‘चिन्ता’ (anxiety) की अनुभूति हुई, तो शायद इस बिन्दु पर जब धर्मचेतना के धुँधले हाशिये पर लुप्त होता गया और दूसरी तरफ मनुष्य का अपना ‘मैं’, अपनी गौरवपूर्ण अस्मिता एक ऐसे संकीर्ण, अहंग्रस्तदायरे में सिकुड़ गई, जहाँ वह अपने भीतर के अँधेरे के समक्ष नितान्त अवश पड़ता गया। क्या मतलब है इस अँधेरे का ? इस प्रश्न के सामने वह बिल्कुल निरुत्तर था। अब मनुष्य विश्व के केन्द्र में नहीं, अपने शून्य के केन्द्र में था-और वहाँ वह बिल्कुल अकेला था।
इसलिए मनुष्य का आत्मबोध अपने होने की चेतना मानव स्वभाव का कोई शाश्वत गुण नहीं है; वह एक प्रक्रिया है जो इतिहास में घटती है-एक दुर्घटना और वरदान दोनों ही। इस प्रक्रिया में आशा और अपशगुन दोनों ही निहिति हैं-स्वतन्त्रता की आशा और अकेलेपन का अपशगुन। मनुष्य की आत्मचेतना दार्शनिक अर्थ में नहीं, जहाँ वह आत्मज्ञान होती है-बल्कि जैविक विकास के अर्थ में-जहाँ मनुष्य को अपने होने, अपने अस्तित्व का बोध होता है-वह आत्मचेतना व्यक्ति की मानसिकता में एक फाँक खींच देती है-और यह फाँक, यह दरार उतनी ही गहरी और विध्वंसात्मक है, जितना वह प्राथमिक पतन जब मानव जाति पहली बार प्रकृति के अभिन्न सम्बन्ध से टूटी थी, विलगित हुई थी और उसने एक सर्वथा उदासीन, सर्वथा भावशून्य विश्व में अपने को नितान्त सीमित, क्षुद्र और क्षणभंगुर पाया था। आज की सभ्यता का संकट और प्रदूषण उस ऐतिहासिक क्षण से शुरू हो गया था, जब मनुष्य प्रकृति से अलग छिटक गया था यह मानव-सभ्यता और मनुष्य की यातना का समान स्रोत है, जो आज हमें घसीटकर ‘अणु युग’ तक ले आया है।
मनुष्य का यह दुहरा अलगाव-प्रकृति से विलगित होना और समाज से अलग टूट जाना-यद्यपि ऐतिहासिक प्रक्रिया के दो अलग-अलग क्षण हैं, किन्तु मनुष्य की चेतना पर उनका प्रभाव बहुत कुछ एक जैसा है-दोनों स्थितियों में ही मनुष्य के भीतर एक भयावह अकेलापन अनाथ हो जाने की कातरता उत्पन्न हो जाती है, वास्तव में जब हम किसी ‘समग्र इकाई’ से टूटते हैं (चाहे वह बच्चे का माँ के गर्भ से अलग होना ही क्यों न हो) तो यह अनाथ-भाव अनिवार्य रूप से हमें आक्रान्त करता है। किन्तु प्रकृति से अलगाव कहीं बहुत गहरे में समाज के अलगाव से भिन्न है; प्रागैतिहासिक-काल का आदिवासी प्रकृति से अलग टूटकर कम-से-कम अपने समूह से जुड़ा रहता है जिसके परिणामस्वरूप उसके निजी अनुभव एक वृहत्तर अनुभव, एक सामूहिक चेतना का ही अंश हैं, जिसमें वह दूसरों के अनुभवों में साझा करता है और दूसरे उसके अनुभव में भाग लेते हैं। किन्तु इससे भिन्न एक सभ्य मनुष्य की आत्मचेतना केवल अपने तक ही केन्द्रित रहती है-उसका निजी व्यक्तित्व एक सम्पूर्ण इकाई है, जिसके भीतर वह समूची बाहरी दुनिया को समेट लेता है-जिसके कारण वह अपने को दूसरों के साथ नहीं, दूसरों के समक्ष या विरुद्ध पाता है। उसका अनुभव यदि दूसरों के अनुभवों में साझा भी करता है, तो अपनी शर्तों पर, एक विराट अनुभव का अंश बनकर नहीं, और जब वह अपने को किसी वृहत्तर इकाई (राज्य तानाशाह या जाति) के प्रति समर्पित करता हूँ, तो भी यह भावना कि ‘मैं अपने को विलय कर रहा हूँ’, उसकी चेतना पर एक याद, एक खरोंच की तरह दगी रहती है।
ऐतिहासिक सभ्य मनुष्य की यह पीड़ा कि वह दूसरों से भिन्न या उनके विरुद्ध है-उस प्रागैतिहासिक मनुष्य की पीड़ा से भिन्न या उनके विरुद्ध है-उस प्रागैतिहासिक मनुष्य की पीड़ा से एक गहरे अर्थ में अलग हो जाती है, जो अपने को प्रकृति के समक्ष तो अकेला पाता है, किन्तु अपने भीतर अकेला महसूस नहीं करता। वास्तव में मिथकों का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वे प्रागैतिहासिक मनुष्य के उस आघात और आतंक को कम कर सकें, जो उसे प्रकृति से सहसा अलग होने पर महसूस हुआ था-और मिथक यह काम केवल एक तरह से ही कर सकते थे-स्वयं प्रकृति और देवताओं का मानवीकरण करके। इस अर्थ में मिथक एक ही समय में मनुष्य के अलगाव को प्रतिबिम्बित करते हैं, और उस अलगाव से जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उससे मुक्ति भी दिलाते हैं। प्रकृति से अभिन्न होने का नॉस्टाल्जिया, प्राथमिक स्मृति की कौंध, शाश्वत और चिरन्तन से पुनः जुड़ने का स्वप्न ये भावनाएँ मिथक को सम्भव बनाने में सबसे सशक्त भूमिका अदा करती हैं। सच पूछें, तो मिथक और कुछ नहीं प्रागैतिहासिक मनुष्य का एक सामूहिक स्वप्न है जो व्यक्ति के स्वप्न की तरह काफी अस्पष्ट, संगतिहीन और संश्लिष्ट भी है। कालान्तर में पुरातन अतीत की ये अस्पष्ट गूँजें, ये धुँधली आकांक्षाएँ एक तर्कसंगत प्रतीकात्मक ढाँचे में ढल जाती हैं और प्राथमिक यथार्थ की पहली, क्षणभंगुर, फिसलती यादें महाकाव्यों (epik) की सुनिश्चित संरचना में गठित होती हैं। मिथक और इतिहास के बीच महाकाव्य एक सेतु है, जो पुरातन स्वप्नों को काव्यात्मक ढाँचे में अवतरित करता है।
किन्तु महाकाव्य के बुनियादी ‘पैटर्न’ और रूप-गठन का आधार अब भी बहुत हद तक वही ‘मिथक-दृष्टि’ है, जिसके सहारे आदि मनुष्य यथार्थ का बोध प्राप्त करता था, बाहरी दुनिया से अपना रिश्ता जोड़ता था। एक-दूसरे से जुड़े तथ्य और घटनाएँ महाकाव्य के लेखक आदि कवि को उतना प्रभावित नहीं करतीं, जितना सामूहिक अवचेतना से जुड़े रूपक (metaphor) उसकी अन्तर्चेतना को अनुप्राणित और आलोकित करते हैं। रूपक से तथ्य और मिथक से तर्क की तरफ बढ़ती हुई मनुष्य की मानसिकता एक तरह से उस ऐतिहासिक विकास (यदि हम उसे ‘विकास’ कह सकें) को ही रेखांकित करती है, जब मनुष्य की सामूहिक अवचेतना धीरे-धीरे व्यक्ति की आत्मचेतना में परिणत होने लगी थी।
महाकाव्य के मिथकीय नायक का अपनी नियति से सम्बन्ध उतना ही समग्र और सहज है, जितना आदिमनुष्य का सम्बन्ध अन्य व्यक्ति से था; वह सामंजस्य और स्वीकृति का रिश्ता है-विरोध और प्रतिरोध का नहीं। इस रिश्ते में एक तरह का अनिवार्यता है, जो उसे निर्मम और कठोर तो बनाती है, लेकिन त्रासद कभी नहीं। ईलियड में आर्खलीस और महाभारत में कर्ण की नियति जीवनधारा का आत्मसमर्पित (आत्मसंकल्पित नहीं) अंग है, जो उसे देवताओं द्वारा रचित वृहत्तर नाटक से जोड़ देती है। मृत्यु का क्षण त्रासद नहीं होता, क्योंकि वह सम्पूर्ण उपलब्धि का क्षण भी है। किन्तु यह बात हैमलेट पर लागू नहीं होती। वह अपने पिता की हत्या के तथ्य के सामने बिल्कुल अकेला है-और यह तथ्य किसी क्रम, किसी पैटर्न, देवताओं के किसी नाटक में फिट नहीं होता-कभी वह हत्या एक घुन की तरह हैमलेट की आत्मा को खाए जाती है। आर्खलीस के जीवन में उसकी मृत्यु एक अनिवार्य परिणति है, जबकि हैमलेट जिन्दगी के साथ झगड़ता हुआ खत्म हो जाता है-बीच बहस में। होमर से शेक्सपियर तक आते-आते मनुष्य की चेतना में आधारभूत परिवर्तन हो चला था-जहाँ पहले वह अपनी प्रकृति नियति से सम्पूर्ण रूप से जुड़ा था, वहाँ कालान्तर में उसकी आत्मा और नियति के बीच एक काली दरार खिंचती गई और यह दरार इतनी गहरी थी कि वह स्वयं अपनी प्रकृति से निर्वासित होता गया। कला में यह परिवर्तन सीधा सृजन-प्रक्रिया में हुआ; पहले कला जहाँ एक अचेतन रचना थी, अब यह रचनात्मक चेतना की अभिव्यक्ति बन गई; किर्केगार्द जिसे ‘सम्पूर्ण सम्भावना’ कहते थे अब वह टूटकर सन्दिग्ध विकल्पों में बँट गई, जिसमें से कोई भी विकल्प मनुष्य चुन सकता था, किन्तु इस चयन का कोई विश्वसनीय दैवी या नैतिक अनुसमर्थन कहीं न था।
यह वह क्षण था, जब मनुष्य का पहली बार अपने ‘मैं’ इगो से साक्षात्कार हुआ, एक ऐसी आत्मभ्रमित चीज जो स्वयं अपने भीतर खंडित थी। पहले जहाँ मनुष्य अपने भीतर समूची वास्तविकता लेकर चलता था, अब वहाँ सिर्फ खोई हुई दुनिया की एक अपाहिज पंगु स्मृति शेष रह गई थी, वह दुनिया खो गई थी, लेकिन मनुष्य उसे भूल नहीं सका था। वास्तव में ‘ईश्वर की मृत्यु’ को लेकर नीत्शे के भयानक आर्तनाद की पीछे यह कातर आकांक्षा छिपी थी कि उस शब्द को दुबारा खोजा जा सके, जो मनुष्य और मिथक को जोड़ता था। एक ऐसे जीवन्त अनुभव का प्रतीक जिसे मनुष्य के अहम बोध ने इतनी बुरी तरह आहत कर दिया था। यह मनुष्य का पतन था। सच कहें, तो दूसरा पतन क्योंकि पहला पतन वह था, जब वह प्रकृति से खंडित हुआ था। मिथक, जो एक समय में मनुष्य के सर्वांगीण, सम्पूर्ण व्यक्तित्व का पोषक था, अब आत्मपीड़ित स्मृतियों के जाले में बदल गया, मनुष्य के खंडित, ज्वरग्रस्त स्वप्नों में उलझा हुआ, जिसे सिर्फ फ्रायड की सूक्तियों और सिद्धान्तों में ही पकड़ा जा सकता था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i