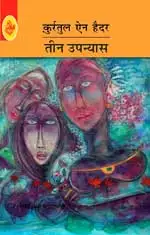|
उपन्यास >> तीन उपन्यास तीन उपन्यासकुर्रतुल ऐन हैदर
|
396 पाठक हैं |
|||||||
अगले जनम मोहे बिटिया न कीजो मामूली नाचने-गानेवाली दो बहनों की कहानी है जो बार-बार मर्दो के छलावों का शिकार होती है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
अगले जनम मोहे बिटिया न कीजो मामूली नाचने-गानेवाली दो बहनों की कहानी है जो बार-बार मर्दो के छलावों का शिकार होती है। फिर भी यह उपन्यास जागीदार घरानों के आर्थिक ही नहीं,भावात्मक खोखलेपन को भी जिस तरह उभारकर सामने लाता है उसकी मिसाल उर्दू साहित्य में मिलना कठिन है। एक जागीदार घराने के आगा फरहाद बकौल खुद पच्चीस साल के बाद भी रश्के-कमर को भूल नहीं पाते और हालात का सितम यह है कि उनके लिए बदोबस्त करते हैं तो कुछेक गजलों का ताकि अगर तुम वापस आओ और मुशायरों में मदऊ (आमंत्रित) किया जाए तो ये गजलें तुम्हारे काम आएँगी। आखिर सबकुछ लूटने के बाद रश्के-कमर के पास बचता है तो बस यही कि कुर्तो की तुरपाई फी कुर्ता दस पैसे...जहाँ उपन्यास का शीर्षक ही हमारे समाज में औरत के हालात पर एक गहरी चोट है,वहीं रश्ते-कमर की छोटी,अपंग बहन जमीलुन्निसा का चरित्र,उसका धीरज उसका व्यक्तियों को पहचानने का गुण और हालात का सामना करने का हौसला मन को सरोबार भी कर जाता है।
खोखलापन और दिखावा-जागीदार तबके की इस त्रासदी को सामने लाने का काम दिलरूबा उपन्यास भी करता है। मगर विरोधाभास यह है कि समाज बदल रहा है और यह तबका भी इस बदलाव से अछूता नहीं रह सकता। यहाँ लेखिका ने प्रतीक इस्तेमाल किया है कि फिल्म उद्योग का जिसके बारे में इस तबके की नौजवान पीढ़ी भी उस विरोध-भावना से मुक्त है जो उन बुजुर्गो में पाई जाती थी। मगर उपन्यास का कथानक कितनी पेचीदगी लिए हुए है इसे स्पष्ट करता है गुलनार बानो का चरित्र-इसी तबके की सताई हुई खातून जो अपना बदला लेने के लिए इस तबके की लड़की को दिलरुबा बनाती है (इस तरह नजरिये की इस तब्दीली का माध्यम भी बनती है) और खुदा का शुक्रिया अदा करती है कि उसने एक तवील मुद्दत के बाद मेरे कलेजे में ठंडक डाली।
तीसरा उपन्यास एक लड़की की जिंदगी है जिसे लेखिका की बेहतरीन तखलीकात में गिना जाता है। यहाँ उन्होंने एक रिफ्यूजी सिंधी लड़की के जरिये पूरे रिफ्यूजी तबके के दुःख-दर्द को उभारा है। उस लड़की के किरदार को लेखिका ने इस तरह पेश किया है कि वह अकेली शख्सियत न रहकर रिफ्यूजी औरत का नुमाइंदा किरदार बन जाती है।
इस तरह कुर्रतुल ऐन हैदर के ये तीनों उपन्यास उनके फन के बेहतरीन नमूनों में गिने जा सकते हैं,साथ ही ये पढ़नेवाले के सामने आज के उर्दू फिक्शन के तेवर को बड़े ही कारगर ढंग से पेश करते हैं।
खोखलापन और दिखावा-जागीदार तबके की इस त्रासदी को सामने लाने का काम दिलरूबा उपन्यास भी करता है। मगर विरोधाभास यह है कि समाज बदल रहा है और यह तबका भी इस बदलाव से अछूता नहीं रह सकता। यहाँ लेखिका ने प्रतीक इस्तेमाल किया है कि फिल्म उद्योग का जिसके बारे में इस तबके की नौजवान पीढ़ी भी उस विरोध-भावना से मुक्त है जो उन बुजुर्गो में पाई जाती थी। मगर उपन्यास का कथानक कितनी पेचीदगी लिए हुए है इसे स्पष्ट करता है गुलनार बानो का चरित्र-इसी तबके की सताई हुई खातून जो अपना बदला लेने के लिए इस तबके की लड़की को दिलरुबा बनाती है (इस तरह नजरिये की इस तब्दीली का माध्यम भी बनती है) और खुदा का शुक्रिया अदा करती है कि उसने एक तवील मुद्दत के बाद मेरे कलेजे में ठंडक डाली।
तीसरा उपन्यास एक लड़की की जिंदगी है जिसे लेखिका की बेहतरीन तखलीकात में गिना जाता है। यहाँ उन्होंने एक रिफ्यूजी सिंधी लड़की के जरिये पूरे रिफ्यूजी तबके के दुःख-दर्द को उभारा है। उस लड़की के किरदार को लेखिका ने इस तरह पेश किया है कि वह अकेली शख्सियत न रहकर रिफ्यूजी औरत का नुमाइंदा किरदार बन जाती है।
इस तरह कुर्रतुल ऐन हैदर के ये तीनों उपन्यास उनके फन के बेहतरीन नमूनों में गिने जा सकते हैं,साथ ही ये पढ़नेवाले के सामने आज के उर्दू फिक्शन के तेवर को बड़े ही कारगर ढंग से पेश करते हैं।
तीन लघु उपन्यास
एक पत्नी के नोट्स
‘एक पत्नी के नोट्स’ वैसे तो आजकल प्रचलित कहानी के वर्गीकरण के हिसाब से लंबी कहानी कहलाएगी; लेकिन यह कहानी से ज़्यादा किसी पॉपुलर फिल्म की स्क्रिप्ट के नज़दीक पड़ती है। हाथ आ जाने पर इस कहानी की रोचकता पाठक को बहा ले जाती है और इस बात की लगभग गारंटी है कि पाठक इसे एक बार में पूरा पढ़े बगैर नहीं छोड़ सकेगा। आजकल किसी भी पत्रिका में छपी लंबी कहानी को पढ़ने से पहले जिस तरह हिम्मत जुटानी पड़ती है, पाठकीय धैर्य और साहस का आवाहन करना पड़ता है, उसके ठीक उलटे इस कहानी में पहले वाक्य से ही मन लगने लगता है। कहानी शहरी पाठक के लिए है। वह सीधे शुरू होती है बिना भूमिका के। कहानी में संदीप है, जो आई.ए.एस. अधिकारी है और उच्च-मध्यवर्ग में संगीत, साहित्य, कला के बारे में जितनी सुरुचि अच्छे सामान्य ज्ञान, बढ़िया पुस्तकों, कैसेटों, म्यूज़िक, कंसर्ट और कल्चर इंडस्ट्री पर अद्यन नज़र रखने से बनती है, उतनी उसके पास है। अच्छी ज़बान हाज़िरजबाबी और आकर्षक व्यक्तित्व ऊपर से। बहरहाल निम्न मध्यवर्ग की गंभीर, सीधी, निश्छल लड़की कविता उसके तेज़ तर्रार ‘इनीशिएटिव’ के आगे समर्पित हो जाती है।
कहानी के विषय में ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है उसकी वस्तु। लेखिका व्यंग्य का इस्तेमाल चरित्राकंन के लिए लगभग एक पैने औज़ार की तरह करती है। साहित्य में जो कुछ भी ‘रोचक’ और ‘लोकप्रिय’ है, उसे मानमूल्यरहित घोषित करना हिंदी में एक आदत-सी है। लेकिन व्यंग्य की एक सी सधी हुई किंतु दबी-दबी सी धार चरित्राकंन के भीतर ही लेखिका के निस्संग और पैने मंतव्य को साफ तौर पर रख देती है।
कहानी के विषय में ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है उसकी वस्तु। लेखिका व्यंग्य का इस्तेमाल चरित्राकंन के लिए लगभग एक पैने औज़ार की तरह करती है। साहित्य में जो कुछ भी ‘रोचक’ और ‘लोकप्रिय’ है, उसे मानमूल्यरहित घोषित करना हिंदी में एक आदत-सी है। लेकिन व्यंग्य की एक सी सधी हुई किंतु दबी-दबी सी धार चरित्राकंन के भीतर ही लेखिका के निस्संग और पैने मंतव्य को साफ तौर पर रख देती है।
-डॉ. प्रणय कृष्ण
भूमिका के बहाने
किसी पुस्तक का पुनर्प्रकाशन न केवल पुस्तक का वरन् लेखक का भी पुनर्जन्म होता है। हिंदी-जगत् में पुस्तकों की बिक्री को लेकर हताशा की स्थिति बनी रहती है। उसके बावजूद अगर कोई पुस्तक पुनर्प्रकाशित होती है तो उसे मैं लेखकीय कौशल की अपेक्षा पाठकों का दबाव और प्रकाशक का सद्भाव मानूँगी।
इन तीनों लघु उपन्यासों या लंबी कहानियों का रचनाकाल व स्थितियाँ अलग-अलग रही हैं। ‘एक पत्नी के नोट्स’ ज़्यादा तसल्ली से लिखी गई रचना है। लखनऊ में हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं दीपक शर्मा और प्रवीण शर्मा। दोनों साहित्यकार हैं। उनके यहाँ दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है। वे क्लासिक से लेकर आधुनिकतम साहित्य, संस्कृति व कला के जानकार हैं। दीपक स्वयं बहुत समर्थ कहानीकार हैं। एक दिन दीपक ने मुझसे कहा, ‘ममता, आप हमेशा औसत स्त्री के बारे में लिखती हैं, जबकि आपको एक प्रबुद्ध स्त्री की त्रासदी के बारे में लिखना चाहिए।’ बात महत्त्वपूर्ण थी। अपन को जम गई। मुझे लगा मैं हमेशा स्त्री के अस्तित्वगत संघर्ष की कथा कहती रही हूँ, जबकि व्यक्तित्वगत संघर्ष कहीं अधिक लंबा और जानलेवा होता है।
‘लड़कियाँ’ उपन्यास की शुरुआत भी दिलचस्प रही। मेरी बड़ी बहन प्रतिभा ने कहा, ‘‘जाने कैसे लिख लेती है तू ! मुझे भी सिखा दे न !’ वह एक बड़ी-सी इमारत ‘करनानी मैंशन’ में रहती थी, जो कलकत्ते के पार्क स्ट्रीट में थी। दीदी उस समय लॉण्ड्री ग्लोब पहनकर वॉश बेसिन साफ कर रही थी। मैंने कहा, ‘दीदी, तू तो अपनी वॉश बेसिन पर एक धब्बा भी बर्दाश्त नहीं करती, लेखक कैसे बनेगी ? मेरे यहाँ देख। किसी को एक रंग के दो मोज़ों का जोड़ा भी मिल जाए तो चमत्कार समझ। आईना धुँधला पड़ जाए तो बदल दिया जाता है, पोंछा नहीं जाता।’ कहने को तो कह दिया, पर मेरी कल्पना चल निकली थी। मुझे उसकी इमारत एक रहस्यलोक लगने लगी थी, जिसके अंदर मुझे प्रवेश सुविधा के लिए घटनास्थल कलकत्ते की जगह मुंबई कर दिया।
‘प्रेम कहानी’ लिखते समय मेरे ज़ेहन पर मॉरीशस का एक मेडिकल छात्र वास्तव में छाया हुआ था, जो अकस्मात् मुझसे टकरा गया था, लेकिन बाद में कभी वादा करने पर भी नहीं आया। युवतर कथा-लेखिका मधु कांकरिया ने कहीं सही लिखा है-‘जो लोग जीवन में नहीं आ पाते, वे ही कहानियों में आ जाते हैं।’ डॉक्टर और अस्पताल की दुनिया मेरी बहुत देखीभाली रही है। मेरी माँ ज़्यादातर रोगग्रस्त रहती थीं और मुझे अपने सभी अहम इम्तिहान अस्पताल से ही जाकर देने पड़े। बी.ए., एम.ए. की तो बात क्या, ग्यारहवीं और इंटर में भी अस्पताल ही मेरी स्टडी रूम रहा है। इस कहानी को अभी और आगे ले जाना था कि मेरा धीरज जवाब दे गया। अब इसका पुनर्लेखन करना शोध-छात्रों के मत्थे एक नये सिरदर्द मढ़ना होगा, इसलिए मैंने इसे अविकल और मूल रूप में ही फिर दे दिया।
सभी रचनाओं के शीर्षक साथी रचनाकार रवीन्द्र कालिया ने रखे हैं। शीर्षक मुझे नहीं सूझता, मैं कोशिश भी नहीं करती।
इस वक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में तीस से भी अधिक शोध-छात्र मेरे कथा-साहित्य पर उच्चतर शोध कार्य कर रहे हैं। इन तीनों क्षीणकाय उपन्यासों की अप्राप्यता को लेकर उनकी बेचैनी मुझ तक पहुँचती रहती है। इसलिए इनका एक जिल्द में आना न केवल उनके लिए, मेरे लिए भी आश्वस्तिदायक है। वरिष्ठ आलोचक गोपाल राय, मधुमेश से लेकर युवा आलोचक प्रणय कृष्ण और कृष्णमोहन ने इन छोटे उपन्यासों पर अपनी बड़ी टिप्पणी दी है, यह तथ्य मेरे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। पाठकों का संवाद और आलोचकों का विवाद किसी भी रचना की जीवनरेखा सिद्ध होता है। ‘एक पत्नी के नोट्स’ ‘लड़कियाँ और प्रेम कहानी को इकट्ठे एक जगह देखना जैसे तीन कालखंडों को गले मिलते देखना है। क्या पता इसी में किसी अगली रचना का सूत्र छुपा हुआ हो।
इन तीनों लघु उपन्यासों या लंबी कहानियों का रचनाकाल व स्थितियाँ अलग-अलग रही हैं। ‘एक पत्नी के नोट्स’ ज़्यादा तसल्ली से लिखी गई रचना है। लखनऊ में हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं दीपक शर्मा और प्रवीण शर्मा। दोनों साहित्यकार हैं। उनके यहाँ दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है। वे क्लासिक से लेकर आधुनिकतम साहित्य, संस्कृति व कला के जानकार हैं। दीपक स्वयं बहुत समर्थ कहानीकार हैं। एक दिन दीपक ने मुझसे कहा, ‘ममता, आप हमेशा औसत स्त्री के बारे में लिखती हैं, जबकि आपको एक प्रबुद्ध स्त्री की त्रासदी के बारे में लिखना चाहिए।’ बात महत्त्वपूर्ण थी। अपन को जम गई। मुझे लगा मैं हमेशा स्त्री के अस्तित्वगत संघर्ष की कथा कहती रही हूँ, जबकि व्यक्तित्वगत संघर्ष कहीं अधिक लंबा और जानलेवा होता है।
‘लड़कियाँ’ उपन्यास की शुरुआत भी दिलचस्प रही। मेरी बड़ी बहन प्रतिभा ने कहा, ‘‘जाने कैसे लिख लेती है तू ! मुझे भी सिखा दे न !’ वह एक बड़ी-सी इमारत ‘करनानी मैंशन’ में रहती थी, जो कलकत्ते के पार्क स्ट्रीट में थी। दीदी उस समय लॉण्ड्री ग्लोब पहनकर वॉश बेसिन साफ कर रही थी। मैंने कहा, ‘दीदी, तू तो अपनी वॉश बेसिन पर एक धब्बा भी बर्दाश्त नहीं करती, लेखक कैसे बनेगी ? मेरे यहाँ देख। किसी को एक रंग के दो मोज़ों का जोड़ा भी मिल जाए तो चमत्कार समझ। आईना धुँधला पड़ जाए तो बदल दिया जाता है, पोंछा नहीं जाता।’ कहने को तो कह दिया, पर मेरी कल्पना चल निकली थी। मुझे उसकी इमारत एक रहस्यलोक लगने लगी थी, जिसके अंदर मुझे प्रवेश सुविधा के लिए घटनास्थल कलकत्ते की जगह मुंबई कर दिया।
‘प्रेम कहानी’ लिखते समय मेरे ज़ेहन पर मॉरीशस का एक मेडिकल छात्र वास्तव में छाया हुआ था, जो अकस्मात् मुझसे टकरा गया था, लेकिन बाद में कभी वादा करने पर भी नहीं आया। युवतर कथा-लेखिका मधु कांकरिया ने कहीं सही लिखा है-‘जो लोग जीवन में नहीं आ पाते, वे ही कहानियों में आ जाते हैं।’ डॉक्टर और अस्पताल की दुनिया मेरी बहुत देखीभाली रही है। मेरी माँ ज़्यादातर रोगग्रस्त रहती थीं और मुझे अपने सभी अहम इम्तिहान अस्पताल से ही जाकर देने पड़े। बी.ए., एम.ए. की तो बात क्या, ग्यारहवीं और इंटर में भी अस्पताल ही मेरी स्टडी रूम रहा है। इस कहानी को अभी और आगे ले जाना था कि मेरा धीरज जवाब दे गया। अब इसका पुनर्लेखन करना शोध-छात्रों के मत्थे एक नये सिरदर्द मढ़ना होगा, इसलिए मैंने इसे अविकल और मूल रूप में ही फिर दे दिया।
सभी रचनाओं के शीर्षक साथी रचनाकार रवीन्द्र कालिया ने रखे हैं। शीर्षक मुझे नहीं सूझता, मैं कोशिश भी नहीं करती।
इस वक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में तीस से भी अधिक शोध-छात्र मेरे कथा-साहित्य पर उच्चतर शोध कार्य कर रहे हैं। इन तीनों क्षीणकाय उपन्यासों की अप्राप्यता को लेकर उनकी बेचैनी मुझ तक पहुँचती रहती है। इसलिए इनका एक जिल्द में आना न केवल उनके लिए, मेरे लिए भी आश्वस्तिदायक है। वरिष्ठ आलोचक गोपाल राय, मधुमेश से लेकर युवा आलोचक प्रणय कृष्ण और कृष्णमोहन ने इन छोटे उपन्यासों पर अपनी बड़ी टिप्पणी दी है, यह तथ्य मेरे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। पाठकों का संवाद और आलोचकों का विवाद किसी भी रचना की जीवनरेखा सिद्ध होता है। ‘एक पत्नी के नोट्स’ ‘लड़कियाँ और प्रेम कहानी को इकट्ठे एक जगह देखना जैसे तीन कालखंडों को गले मिलते देखना है। क्या पता इसी में किसी अगली रचना का सूत्र छुपा हुआ हो।
-ममता कालिया
एक पत्नी के नोट्स
जिन लोगों के जीवन में प्रेम और विवाह अकस्मात् अनायास आते हैं उन्हें उसके निर्वाह में उतनी ही सायास मेहनत करनी पड़ती है, जितनी उन लोगों को जिनके विवाह अखबारों के इश्तहार तय करते हैं अथवा रिश्तेदार। यह बात जितनी कविता के लिए सच थी उतनी ही संदीप के लिए भी। लेकिन संदीप किसी बात को इतनी सहजता से स्वीकार कर ले, यह कैसे हो सकता था ?
संदीप एक प्रबुद्ध व्यक्ति था। उसके पिता प्रसिद्ध साहित्यकार थे। होश सँभालते ही उसने अपने घर में बेशुमार किताबें देखीं। बल्कि यह कहना ठीक होगा कि उसने किताबों के रास्ते जीवन के सब फैसले किए थे। एम.ए. में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाने पर वह लेक्चचर भी बन सकता था, पर लेखक पिता की हार्दिक इच्छा थी कि वह सिविल सर्विसेज़ प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा परखे। बिना किसी विशेष श्रम के पहली बार ही संदीप आई.ए.एस. में भी उत्तीर्ण हो गया। पिता को बड़ा संतोष और गर्व हुआ पर उसकी नियुक्ति से पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। विरासत में संदीप के लिए वे पुस्तकों की अपार संपदा छोड़ गए और अपनी आकांक्षाएँ। संदीप ने दोनों का सम्मान किया। उसने एक तरफ लोक-प्रशासन के पेच और पहलू समझे तो दूसरी तरफ विश्व के महान् साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन कर डाला। संदीप अगर प्राध्यापक बनता तो एक विशिष्ट बुद्धिजीवी के रूप में सम्मान पाता, किंतु दिवंगत पिता की इच्छा की खातिर उसने अफसरी अपना ली।
धीरे धीरे उसकी टेबल पर पुस्तकों की जगह फाइलों ने ले ली। उसके दिमाग में कंप्यूटर की सी तेज़ी थी। इसका अंदाज़ उसके विभाग को थोड़ा-थोड़ा तब हुआ जब यह पाया गया कि कहीं भी फोन करने के लिए संदीप डायरेक्टरी का इस्तेमाल नहीं करता उसे दो हज़ार से भी ज़्यादा टेलीफोन नंबर मौखिक याद थे। किसी भी विभाग का काम समझने में उसे मुश्किल से कुछ घंटे दरकार होते। वह विभाग की गड़बड़ रग पर उँगली रख देता। वह युद्ध-स्तर पर काम निपटाता और किसी को भी बुलाकर साहित्य-चर्चा द्वारा अपना मनोरंजन कर लेता। उसकी पी.ए. एक मूर्ख किस्म की फैशनेबल लड़की थी। वह शालीन भंगिमा में अपने बॉस के उद्गार सुनती रहती और बोर होती। अंत में एक गहरी साँस लेकर वह पर्स से काला चश्मा निकाल लेती और घर जाते-जाते मन ही मन अपने अनोखे अफसर को इस विलंब के लिए क्षमा भी कर देती।
संदीप का दिल-दिमाग हर समय साहित्य से आंदोलित रहता। उसकी निजी लाइब्रेरी में प्राचीन, समकालीन सभी प्रकार की पुस्तकें थीं। सही मौके पर सटीक उद्धरण देना उसकी विशेषता थी। हाज़िरजवाबी सांस्कृतिक सूझ-बूझ, शायराना तबीयत और साहित्यिक रुचियों के कारण वह शहर में लोकप्रिय हो गया। मंत्रिमंडल से लेकर मित्र-मंडली तक में उसका स्वागत होने लगा। इन स्थितियों में वह अपने को बेहद प्रतिभाशाली, भाग्यशाली और प्रबुद्ध समझने के लिए बाध्य हो गया।
मार्च के एक सुहाने दिन, जब सड़कें अनाम फूलों से सजी-सँवरी थीं, हवा में हलकी खुनकी शेष थी और दफ्तर के वित्त वर्ष का काम उसके काबू में था, वह प्रेम में पड़ गया। दरअसल उस लड़की को एक अरसे से वह आते जाते देख चुका था। लगता था, संदीप का दफ्तर जाने का वक्त और लड़की का विश्वविद्यालय जाने का वक्त एक ही था। एक खास मोड़ पर उसे वह लड़की हाथ में डायरी कलात्मक कदमों से रिक्शा स्टैंड तक आती दिखाई देती। यह इतना नियमित साक्षात्कार था कि अगर किसी दिन वह उसे न दिखाई देती, तो वह वहीं गुलमोहर के नीचे कार रोक देता। जैसे ही दूर से वह लड़की उसे आती दिखाई देती, वह झटके से कार मोड़कर दूसरी दिशा से दफ्तर चला जाता। वह अभी न उसका नाम जानता था, न पता, पर उसे उस लड़की का अकेलापन बहुत आकर्षित करता था, वह लंबे, भरे-भरे जिस्म वाली लड़की थी, जो चौड़े-चौड़े बॉर्डर की बँगला साड़ियाँ पहनती थी। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी थीं, विस्फारित-सी जैसे प्रतिदिन उसे जीवन एक चमत्कार दिखाई देता हो। संदीप को उसका निष्पलक भोलापन बरबस खींचता था। उस लड़की के व्यक्तित्व में एक संत की सी सहजता और सादगी थी, जो कौमार्य की गरिमा के साथ कुछ इस तरह रच-बस गई थी कि उसके चेहरे पर एक खास तेजस्विता बनी रहती थी।
मार्च के उस दिन संदीप मस्ती में था। उसका मन अतिरिक्त काव्यात्मक हो रहा था। तभी उसने देखा, वही लड़की रिक्शा स्टैंड पर कुछ-कुछ परेशान, कुछ-कुछ क्लांत खड़ी है। स्टैंड पर एक भी रिक्शा नहीं था। अनायास ही उसने कार रोक दी और अत्यंत शिष्टता से कहा, ‘‘मैं आपसे परिचित तो नहीं, अपरिचित भी नहीं हूँ। मैं भी विश्वविद्यालय की तरफ जा रहा था। आपको मेरी शालीनता पर यकीन हो तो साथ चल सकती हैं।’’
किसी नवयुवक से इतनी साफ-सुथरी जबान कविता ने पहली बार सुनी थी। न जाने वह रिक्शा न मिलने की परेशानी थी या कोई रूहानी खिंचाव, वह कार में बैठ गई। संदीप ने निःशब्द उसे गंतव्य तक पहुँचा दिया और कविता के उतरने के पहले बड़े सलीके से अपनी गहन आवाज़ में बोला, ‘‘मैं आपका नाम इसलिए नहीं जानना चाहता, क्योंकि आप अजनबी-सी हैं, मगर गैर नहीं लगती हैं। सिर्फ एक छोटा सा शेर सुनती जाइए :
संदीप एक प्रबुद्ध व्यक्ति था। उसके पिता प्रसिद्ध साहित्यकार थे। होश सँभालते ही उसने अपने घर में बेशुमार किताबें देखीं। बल्कि यह कहना ठीक होगा कि उसने किताबों के रास्ते जीवन के सब फैसले किए थे। एम.ए. में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाने पर वह लेक्चचर भी बन सकता था, पर लेखक पिता की हार्दिक इच्छा थी कि वह सिविल सर्विसेज़ प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा परखे। बिना किसी विशेष श्रम के पहली बार ही संदीप आई.ए.एस. में भी उत्तीर्ण हो गया। पिता को बड़ा संतोष और गर्व हुआ पर उसकी नियुक्ति से पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। विरासत में संदीप के लिए वे पुस्तकों की अपार संपदा छोड़ गए और अपनी आकांक्षाएँ। संदीप ने दोनों का सम्मान किया। उसने एक तरफ लोक-प्रशासन के पेच और पहलू समझे तो दूसरी तरफ विश्व के महान् साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन कर डाला। संदीप अगर प्राध्यापक बनता तो एक विशिष्ट बुद्धिजीवी के रूप में सम्मान पाता, किंतु दिवंगत पिता की इच्छा की खातिर उसने अफसरी अपना ली।
धीरे धीरे उसकी टेबल पर पुस्तकों की जगह फाइलों ने ले ली। उसके दिमाग में कंप्यूटर की सी तेज़ी थी। इसका अंदाज़ उसके विभाग को थोड़ा-थोड़ा तब हुआ जब यह पाया गया कि कहीं भी फोन करने के लिए संदीप डायरेक्टरी का इस्तेमाल नहीं करता उसे दो हज़ार से भी ज़्यादा टेलीफोन नंबर मौखिक याद थे। किसी भी विभाग का काम समझने में उसे मुश्किल से कुछ घंटे दरकार होते। वह विभाग की गड़बड़ रग पर उँगली रख देता। वह युद्ध-स्तर पर काम निपटाता और किसी को भी बुलाकर साहित्य-चर्चा द्वारा अपना मनोरंजन कर लेता। उसकी पी.ए. एक मूर्ख किस्म की फैशनेबल लड़की थी। वह शालीन भंगिमा में अपने बॉस के उद्गार सुनती रहती और बोर होती। अंत में एक गहरी साँस लेकर वह पर्स से काला चश्मा निकाल लेती और घर जाते-जाते मन ही मन अपने अनोखे अफसर को इस विलंब के लिए क्षमा भी कर देती।
संदीप का दिल-दिमाग हर समय साहित्य से आंदोलित रहता। उसकी निजी लाइब्रेरी में प्राचीन, समकालीन सभी प्रकार की पुस्तकें थीं। सही मौके पर सटीक उद्धरण देना उसकी विशेषता थी। हाज़िरजवाबी सांस्कृतिक सूझ-बूझ, शायराना तबीयत और साहित्यिक रुचियों के कारण वह शहर में लोकप्रिय हो गया। मंत्रिमंडल से लेकर मित्र-मंडली तक में उसका स्वागत होने लगा। इन स्थितियों में वह अपने को बेहद प्रतिभाशाली, भाग्यशाली और प्रबुद्ध समझने के लिए बाध्य हो गया।
मार्च के एक सुहाने दिन, जब सड़कें अनाम फूलों से सजी-सँवरी थीं, हवा में हलकी खुनकी शेष थी और दफ्तर के वित्त वर्ष का काम उसके काबू में था, वह प्रेम में पड़ गया। दरअसल उस लड़की को एक अरसे से वह आते जाते देख चुका था। लगता था, संदीप का दफ्तर जाने का वक्त और लड़की का विश्वविद्यालय जाने का वक्त एक ही था। एक खास मोड़ पर उसे वह लड़की हाथ में डायरी कलात्मक कदमों से रिक्शा स्टैंड तक आती दिखाई देती। यह इतना नियमित साक्षात्कार था कि अगर किसी दिन वह उसे न दिखाई देती, तो वह वहीं गुलमोहर के नीचे कार रोक देता। जैसे ही दूर से वह लड़की उसे आती दिखाई देती, वह झटके से कार मोड़कर दूसरी दिशा से दफ्तर चला जाता। वह अभी न उसका नाम जानता था, न पता, पर उसे उस लड़की का अकेलापन बहुत आकर्षित करता था, वह लंबे, भरे-भरे जिस्म वाली लड़की थी, जो चौड़े-चौड़े बॉर्डर की बँगला साड़ियाँ पहनती थी। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी थीं, विस्फारित-सी जैसे प्रतिदिन उसे जीवन एक चमत्कार दिखाई देता हो। संदीप को उसका निष्पलक भोलापन बरबस खींचता था। उस लड़की के व्यक्तित्व में एक संत की सी सहजता और सादगी थी, जो कौमार्य की गरिमा के साथ कुछ इस तरह रच-बस गई थी कि उसके चेहरे पर एक खास तेजस्विता बनी रहती थी।
मार्च के उस दिन संदीप मस्ती में था। उसका मन अतिरिक्त काव्यात्मक हो रहा था। तभी उसने देखा, वही लड़की रिक्शा स्टैंड पर कुछ-कुछ परेशान, कुछ-कुछ क्लांत खड़ी है। स्टैंड पर एक भी रिक्शा नहीं था। अनायास ही उसने कार रोक दी और अत्यंत शिष्टता से कहा, ‘‘मैं आपसे परिचित तो नहीं, अपरिचित भी नहीं हूँ। मैं भी विश्वविद्यालय की तरफ जा रहा था। आपको मेरी शालीनता पर यकीन हो तो साथ चल सकती हैं।’’
किसी नवयुवक से इतनी साफ-सुथरी जबान कविता ने पहली बार सुनी थी। न जाने वह रिक्शा न मिलने की परेशानी थी या कोई रूहानी खिंचाव, वह कार में बैठ गई। संदीप ने निःशब्द उसे गंतव्य तक पहुँचा दिया और कविता के उतरने के पहले बड़े सलीके से अपनी गहन आवाज़ में बोला, ‘‘मैं आपका नाम इसलिए नहीं जानना चाहता, क्योंकि आप अजनबी-सी हैं, मगर गैर नहीं लगती हैं। सिर्फ एक छोटा सा शेर सुनती जाइए :
किसलिए जलाए हैं अब दिए किनारों पर,
अब तो डूबने वाला डूब भी चुका होगा।
अब तो डूबने वाला डूब भी चुका होगा।
लड़की अंदर तक झनझना गई। उसके कानों में वंशी से लेकर शहनाई तक सभी वाद्यबज उठे। एक क्षण रुककर संदीप ने कार का दरवाज़ा खोल दिया।
कविता उतर गई। दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, ‘‘थैंक्यू फॉर एवरीथिंग मिस्टर सिंह !’’
अब चौंकने की बारी संदीप की थी, ‘‘आप मुझे जानती हैं ?’’
‘‘आपको कौन नहीं जानता ? मेरा नाम कविता है।’’
कविता चली गई।
संदीप के कानों में कविता की अस्फुट आवाज़ सारे दिन गूँजती रही, ‘आपको कौन नहीं जानता, आपको...।’
आत्मविश्वास संदीप के अंदर पहले ही कूट-कूटकर भरा था, इस बात से उसका अहं इतना प्रसन्न और प्रफुल्लित हुआ कि उसे लगा, उसकी तलाश खत्म हुई। इस लड़की के इतने संक्षिप्त सान्निध्य से उसे कई स्तरों पर आह्लाद हुआ। एक तो यही कि कविता के बारे में उसके सभी अनुमान सही निकले। वह साहित्य की छात्रा थी। उसके पिता निम्न मध्य वर्ग के अवकाश प्राप्त हैडमास्टर थे। वह चार बहनों में सबसे बड़ी थी, भाई उससे बड़ा था और विवाहित। जीवन के बारे में उसका दृष्टिकोण बेहद आदर्शवादी और आस्थापूर्ण था। ये सारी स्थितियाँ संदीप के उस भाव का भी पोषण करती थीं, जिसके तहत वह हमेशा अपने आपको दूसरों से श्रेष्ठ मानता आया था। कविता की पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक हैसियत ने उसे एक अन्वेषक के आनंद से भर दिया। उसे लगा, वह कोलंबस है और कविता अमेरिका।
संदीप जानता था कि इतनी गंभीर, सीधी और निश्छल लड़की को गंभीरता, सादगी, आदर्शवाद और आस्था के स्तर पर ही जीता जा सकता है। उसने अपना व्यवहार लड़की की अपेक्षाओं के अनुकूल ही रखा। उसे यह सोचना भी अच्छा लगा कि उसका प्रेम-प्रसंग विशिष्ट गरिमा से मंडित है-साधारण लड़कों के निम्नस्तरीय प्रेम-प्रसंगों से एकदम अलग। इस तरह संदीप के दिमाग में कविता की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, अपने पद की प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई, जिसके रहते ही उसके व्यवहार में इतना संयम और विवेक था। उसने अपना प्रेम-निवेदन काव्यात्मक बना दिया। जैसे एक दिन उसने कविता से कहा :
कविता उतर गई। दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, ‘‘थैंक्यू फॉर एवरीथिंग मिस्टर सिंह !’’
अब चौंकने की बारी संदीप की थी, ‘‘आप मुझे जानती हैं ?’’
‘‘आपको कौन नहीं जानता ? मेरा नाम कविता है।’’
कविता चली गई।
संदीप के कानों में कविता की अस्फुट आवाज़ सारे दिन गूँजती रही, ‘आपको कौन नहीं जानता, आपको...।’
आत्मविश्वास संदीप के अंदर पहले ही कूट-कूटकर भरा था, इस बात से उसका अहं इतना प्रसन्न और प्रफुल्लित हुआ कि उसे लगा, उसकी तलाश खत्म हुई। इस लड़की के इतने संक्षिप्त सान्निध्य से उसे कई स्तरों पर आह्लाद हुआ। एक तो यही कि कविता के बारे में उसके सभी अनुमान सही निकले। वह साहित्य की छात्रा थी। उसके पिता निम्न मध्य वर्ग के अवकाश प्राप्त हैडमास्टर थे। वह चार बहनों में सबसे बड़ी थी, भाई उससे बड़ा था और विवाहित। जीवन के बारे में उसका दृष्टिकोण बेहद आदर्शवादी और आस्थापूर्ण था। ये सारी स्थितियाँ संदीप के उस भाव का भी पोषण करती थीं, जिसके तहत वह हमेशा अपने आपको दूसरों से श्रेष्ठ मानता आया था। कविता की पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक हैसियत ने उसे एक अन्वेषक के आनंद से भर दिया। उसे लगा, वह कोलंबस है और कविता अमेरिका।
संदीप जानता था कि इतनी गंभीर, सीधी और निश्छल लड़की को गंभीरता, सादगी, आदर्शवाद और आस्था के स्तर पर ही जीता जा सकता है। उसने अपना व्यवहार लड़की की अपेक्षाओं के अनुकूल ही रखा। उसे यह सोचना भी अच्छा लगा कि उसका प्रेम-प्रसंग विशिष्ट गरिमा से मंडित है-साधारण लड़कों के निम्नस्तरीय प्रेम-प्रसंगों से एकदम अलग। इस तरह संदीप के दिमाग में कविता की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, अपने पद की प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई, जिसके रहते ही उसके व्यवहार में इतना संयम और विवेक था। उसने अपना प्रेम-निवेदन काव्यात्मक बना दिया। जैसे एक दिन उसने कविता से कहा :
‘‘तुम्हारा चेहरा उस दिन का
मेरा सबसे बड़ा आश्चर्य है।
मेरा सबसे बड़ा आश्चर्य है।
संदीप आजकल रोज़ कविता को छोड़ने विश्वविद्यालय तक जाता। रात घर पर वह अपने बड़े फ्लैट के एकांत कमरों में कविता के प्रति मौन संदेश संबोधित करता रहता। उसे यह सोचकर पुलक होती कि जल्द ही ये कमरे सूने नहीं रहेंगे। इनकी हर दीवार पर मंगलचिह्न की तरह कविता की परछाईं होगी। सुबह कविता को पहलू में बिठाकर ड्राइव करते हुए वह कह उठता :
‘‘आटे में थोड़े नमक की तरह
तुम्हारी याद
मुझे स्वाद से भर देगी।
तुम्हारी याद
मुझे स्वाद से भर देगी।
संदीप के मुँह से निकला हर वाक्य कविता को झकझोर डालता। उसे लगता, वह लड़की की जगह एक कलाकृति बनती जा रही है। उसकी आँखें और अधिक गहन, संवेदनशील हो आईं वे अब चकित ही नहीं, विस्मित लगती थीं। उसे अपने भाग्य पर बहुत गर्व हुआ। विश्वविद्यालय में लड़कियों के बीच उसका रुतबा बढ़ गया था। उसके पास शहर का सबसे स्मार्ट आई.ए.एस. प्रेमी था। जबकि क्लास की बाकी लड़कियाँ इंजीनियर, डॉक्टर तक को दिल देने को तैयार बैठी थीं।
साहित्य की छात्रा होना एक बात थी, साहित्य की विषयवस्तु बनाई जाना नितांत दूसरी। कविता को हिंदी साहित्य की थोड़ी-बहुत जानकारी तो थी, पर साहित्य उसके लिए जीवन का पर्याय नहीं था। अकसर उसे यह भी न पता होता कि संदीप किस कवि की रचना से उसे अंलकृत कर रहा है। वह अपने विस्मित विस्फारित नेत्रों की एक झपक से इस सौगात को स्वीकार कर लेती। पाठ्य-पुस्तकों से हटकर वह केवल शरत्-चन्द्र रवीन्द्र संगीत और छायावादी कवियों तक पहुँच पाई थी। उसमें वह हाज़िरजवाबी नहीं थी कि संदीप के संबोधनों का उसी स्तर पर जवाब दे सके, पर उसकी यह असमर्थता ही उसकी प्रियता भी थी। संदीप से परिचय के बाद उसका जीवन वही होते हुए भी वही नहीं रहा था। उसमें रूप, रस और रंग आ मिला था। प्रेम की तरलता उसके अंग-अंग में एक सिम्फनी बनकर प्राप्त हो गई। घर की बेमज़ा दौड़ भाग में वह यकायक एक तटस्थ दर्शक बन गई। उसे अपनी बहनें बेसलीका लगने लगीं और माता-पिता महाबोर। उसकी समस्त चेतना संदीप के आसपास मँडराने लगी। संदीप का व्यवहार उसकी भाषा अभिव्यक्ति, उसका पद और कद सब उसे एक आश्चर्यलोक में पहुँचा देता, जहाँ वह महज़ अपनी बड़ी-बड़ी आँखें टिकाकर संदीप को सुनती रहती। बोलने का शौक संदीप को शुरू से था, प्रेयसी को श्रोता के रूप में पाकर उसे जैसे पंख मिल गए। गोमती के किनारे चांदनी रातों में कविता का मुख अपने हाथों में लेकर वह कह उठता :
साहित्य की छात्रा होना एक बात थी, साहित्य की विषयवस्तु बनाई जाना नितांत दूसरी। कविता को हिंदी साहित्य की थोड़ी-बहुत जानकारी तो थी, पर साहित्य उसके लिए जीवन का पर्याय नहीं था। अकसर उसे यह भी न पता होता कि संदीप किस कवि की रचना से उसे अंलकृत कर रहा है। वह अपने विस्मित विस्फारित नेत्रों की एक झपक से इस सौगात को स्वीकार कर लेती। पाठ्य-पुस्तकों से हटकर वह केवल शरत्-चन्द्र रवीन्द्र संगीत और छायावादी कवियों तक पहुँच पाई थी। उसमें वह हाज़िरजवाबी नहीं थी कि संदीप के संबोधनों का उसी स्तर पर जवाब दे सके, पर उसकी यह असमर्थता ही उसकी प्रियता भी थी। संदीप से परिचय के बाद उसका जीवन वही होते हुए भी वही नहीं रहा था। उसमें रूप, रस और रंग आ मिला था। प्रेम की तरलता उसके अंग-अंग में एक सिम्फनी बनकर प्राप्त हो गई। घर की बेमज़ा दौड़ भाग में वह यकायक एक तटस्थ दर्शक बन गई। उसे अपनी बहनें बेसलीका लगने लगीं और माता-पिता महाबोर। उसकी समस्त चेतना संदीप के आसपास मँडराने लगी। संदीप का व्यवहार उसकी भाषा अभिव्यक्ति, उसका पद और कद सब उसे एक आश्चर्यलोक में पहुँचा देता, जहाँ वह महज़ अपनी बड़ी-बड़ी आँखें टिकाकर संदीप को सुनती रहती। बोलने का शौक संदीप को शुरू से था, प्रेयसी को श्रोता के रूप में पाकर उसे जैसे पंख मिल गए। गोमती के किनारे चांदनी रातों में कविता का मुख अपने हाथों में लेकर वह कह उठता :
‘‘सुना है अब नदियाँ नहीं सूखेंगी।
इधर आओ।
चाँदनी का स्कार्फ
तुम्हारे चेहरे पर बाँध दूँ।
इधर आओ।
चाँदनी का स्कार्फ
तुम्हारे चेहरे पर बाँध दूँ।
कभी-कभी वह उसे ‘गीत गोविंद’ के छंद सुना डालता। संस्कृत न जानते हुए भी कविता उस छंद-चयन पर बेहद लजा उठती। उसे वास्तव में लगता, वह राधा है और संदीप मदनातुर कृष्ण, जब वह गा उठता :
‘‘रतिसुख सारे गतमभिसारे मदन-मनोहर-वेशम्।
न कुरु नितंबिनि गमन विलंबिन मनुसरतं हृदयेशम्।
धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने बनमाली,
पीन-पयोधर-परिसर-मर्दन-चंचल-कर-युगशाली।
न कुरु नितंबिनि गमन विलंबिन मनुसरतं हृदयेशम्।
धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने बनमाली,
पीन-पयोधर-परिसर-मर्दन-चंचल-कर-युगशाली।
संदीप की मंशा समझने के बावजूद कविता ने कभी उसे शब्द-स्पर्श से आगे नहीं बढ़ने दिया। आदर्शवादिता के साथ-साथ उसमें भीरुता भी समाई हुई थी। बेहद डरते-डरते वह संदीप के साथ कहीं बाहर निकलती, फिर घबराकर वक्त से पहले ही घर वापस चलने की ज़िद करती।
संदीप पूछता, ‘‘किसके अपने या तुम्हारे ?’’
कविता कहती, ‘‘अपने-अपने।’’
एक दो बार जब संदीप ने उठने में देर लगाई, उसे रोकने का मनुहार किया, वह उतावली में खुद रिक्शा करके अकेले घर चली गई। उसके ज़ेहन में यकायक सिंड्रैला जैसी कोई घंटी बज उठती और वह ऐन उस क्षण उठ जाती, जब संदीप का दिल, दिमाग, देह उसे पूरी तरह ढाँप लेना चाहता था। ऐसे समय स्टियरिंग पर माथा टेक संदीप अवश कह उठता :
संदीप पूछता, ‘‘किसके अपने या तुम्हारे ?’’
कविता कहती, ‘‘अपने-अपने।’’
एक दो बार जब संदीप ने उठने में देर लगाई, उसे रोकने का मनुहार किया, वह उतावली में खुद रिक्शा करके अकेले घर चली गई। उसके ज़ेहन में यकायक सिंड्रैला जैसी कोई घंटी बज उठती और वह ऐन उस क्षण उठ जाती, जब संदीप का दिल, दिमाग, देह उसे पूरी तरह ढाँप लेना चाहता था। ऐसे समय स्टियरिंग पर माथा टेक संदीप अवश कह उठता :
‘‘दूरी तुम दूर नहीं, मेरी पुकार ही अक्षम है,
कोई विस्तार दृष्टि मुझमें ही कम है।
कोई विस्तार दृष्टि मुझमें ही कम है।
कुछ दिनों के लिए संदीप को अपने सारे दोस्त भूल गए। वैसे भी, वह जो भी काम करता, पूरी तल्लीनता से। इस वक्त अपनी चेतना और स्फूर्ति का सर्वश्रेष्ठ भाग उसने कविता को सौंप दिया था। विचारों की उड़ान में कभी उसे लगता, वह ब्राउनिंग है और कविता एलिज़बेथ, जिसे उसे विम्पोल स्ट्रीट से ले भागना है। कभी वह महसूस करता, वह राँझा है और कविता हीर, बाकी सारी दुनिया उसे कैदों नज़र आती।
घर पर संदीप के लिए एक से एक समृद्ध परिवारों की लड़कियों के रिश्तें आ रहे थे। सभी लड़कियाँ घोषित रूप से सुंदर, सुशील, सुशिक्षित और गृहकार्य में दक्ष थीं। सभी के पिता संपन्न थे और आई.ए.एस. दामाद खरीदने की हैसियत रखते थे। संदीप की माँ इन सब प्रस्तावों से गौरवान्वित होतीं, लेकिन वह बेटे की इच्छाओं का सम्मान करना जानती थीं। वे चुप रहतीं। उनकी अनुभवी आँखों को पता था, उनका सुंदर, कुशाग्र पुत्र अब तक ज़रूर किसी न किसी ठाँव अपने मन की नाव बाँध चुका होगा, नहीं तो यों ही बेवजह वह इतना खुश न दिखाई देता, इसलिए एक दिन जब बिना किसी भूमिका के बेटे ने उन्हें बताया कि वह कविता से शादी का फैसला कर चुका है, माँ ने कोई फसाद खड़ा नहीं किया, चुपचाप गरिमापूर्ण ढंग से विवाह में शामिल हो गईं। उनकी आयु अब मात्र आशीर्वाद देने की थी।
घर पर संदीप के लिए एक से एक समृद्ध परिवारों की लड़कियों के रिश्तें आ रहे थे। सभी लड़कियाँ घोषित रूप से सुंदर, सुशील, सुशिक्षित और गृहकार्य में दक्ष थीं। सभी के पिता संपन्न थे और आई.ए.एस. दामाद खरीदने की हैसियत रखते थे। संदीप की माँ इन सब प्रस्तावों से गौरवान्वित होतीं, लेकिन वह बेटे की इच्छाओं का सम्मान करना जानती थीं। वे चुप रहतीं। उनकी अनुभवी आँखों को पता था, उनका सुंदर, कुशाग्र पुत्र अब तक ज़रूर किसी न किसी ठाँव अपने मन की नाव बाँध चुका होगा, नहीं तो यों ही बेवजह वह इतना खुश न दिखाई देता, इसलिए एक दिन जब बिना किसी भूमिका के बेटे ने उन्हें बताया कि वह कविता से शादी का फैसला कर चुका है, माँ ने कोई फसाद खड़ा नहीं किया, चुपचाप गरिमापूर्ण ढंग से विवाह में शामिल हो गईं। उनकी आयु अब मात्र आशीर्वाद देने की थी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i