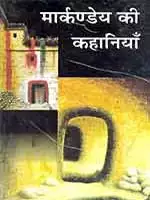|
कहानी संग्रह >> मार्कण्डेय की कहानियाँ मार्कण्डेय की कहानियाँमार्कण्डेय
|
242 पाठक हैं |
|||||||
मार्कण्डेय की इन सात कहानियों में धार्मिक अंधविश्वास, शोषण और अनाचार के परिवेश को उजागर किया गया है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रस्तुत संकलन में मार्कण्डेय के अब तक प्रकाशित सात कहानी संग्रह शामिल
हैं।
कहना न होगा कि स्वतंत्रता के बाद लिखी गयी इन कहानियों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ है। देश-विदेश में भी इनके अनुवादों पर वहाँ के आलोचकों ने लेख एवं समीक्षाएँ लिखी हैं।
अत्यन्त सहज वाचन और शिल्पगत नवीनता के कारण इन कहानियों में चिह्नित समकालीन संदर्भ भारतीय जीवन की वास्तविकताओं को लोगों के सामने ला खड़ा करते हैं। आदर्श और बाह्य मान्यताओं वाली दृष्टि से देखे जाने के कारण संघर्ष और बदलाव की जो बातें हवा में उठायी जा रही थीं उनके सामने उन कहानियों ने एक नया दृश्य ला खड़ा किया। अंधकार, अंधविश्वास, शोषण और अनाचार के परिवेश को उजागर करने के कारण इन कहानियों को लोगो ने एक उपलब्धि की तरह स्वीकार किया। इस संकलन में ‘पान-फूल’, ‘महुए का पेड़’, ‘हंसा जाई अकेला’, ‘भूदान’, ‘माही’, ‘सहज और शुभ’ तथा ‘बीच’ के लोग नामक पुस्तकें शामिल हैं।
कहना न होगा कि स्वतंत्रता के बाद लिखी गयी इन कहानियों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ है। देश-विदेश में भी इनके अनुवादों पर वहाँ के आलोचकों ने लेख एवं समीक्षाएँ लिखी हैं।
अत्यन्त सहज वाचन और शिल्पगत नवीनता के कारण इन कहानियों में चिह्नित समकालीन संदर्भ भारतीय जीवन की वास्तविकताओं को लोगों के सामने ला खड़ा करते हैं। आदर्श और बाह्य मान्यताओं वाली दृष्टि से देखे जाने के कारण संघर्ष और बदलाव की जो बातें हवा में उठायी जा रही थीं उनके सामने उन कहानियों ने एक नया दृश्य ला खड़ा किया। अंधकार, अंधविश्वास, शोषण और अनाचार के परिवेश को उजागर करने के कारण इन कहानियों को लोगो ने एक उपलब्धि की तरह स्वीकार किया। इस संकलन में ‘पान-फूल’, ‘महुए का पेड़’, ‘हंसा जाई अकेला’, ‘भूदान’, ‘माही’, ‘सहज और शुभ’ तथा ‘बीच’ के लोग नामक पुस्तकें शामिल हैं।
भूमिका
इन कहानियों का समय आजादी के ठीक बाद का है, जब साहित्य में गतिरोध की
चर्चा हो रही थी। अभिप्राय यह नहीं कि साहित्य लिखा कम जा रहा था बल्कि यह
कि वह अपने समय तथा जीवन संदर्भों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। ऐसा
लगता था जैसे वह किन्हीं पूर्व मान्यताओं के कारण अपने देश के सामाजिक
संदर्भों और वास्तविकताओं की उपेक्षा कर रहा हो। कथा-संदर्भों के लिए तो
तो यह काल और भी उलझनों भरा था। अज्ञेय और जैनेन्द्र ने कथा-रचना के
क्षेत्र से अपने को समेटना शुरू कर दिया था। व्यक्ति की आंतरिकता का विघटन
दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और नये सृजन के लिए अब उसमें कुछ भी
संभावनायें शेष नहीं रह गयी थीं। प्रगतिशील कथाकारों का रोमानी यथार्थवाद
आजादी के साथ और भी फीका पड़ गया। वे नयी परिस्थितियों के मूल्यांकन में
चूक गये थे और नयी वास्तविकताओं की उपेक्षा कर कल्पना की सृष्टि कर रहे
थे।
नयी कहानी का उदय इसी उलझे हुए सामाजिक संदर्भ में स्वाधीनता की सहज मान्यता के कारण, आशा भरे उत्साह के बीच हुआ। शुरू के प्रगतिशील दौर की जनोन्मुखी दृष्टि इसे विरासत में मिली थी। इस काल-खण्ड में नये–नये आने वाले लेखकों ने प्रगतिशील कहानियों की मुख्य कमजोरी को भलीभाँति समझा था। यही कारण था कि उन्हें कि उन्होंने अपनी कथा रचना का मूलाधार वहीं खड़ा किया जिसकी उपेक्षा के कारण व्यक्तिवादी रचनाकार और प्रगतिशाल दोनों फीके पड़ गये थे।
सामाजिक संदर्भों का वास्तविक चित्रण नये कथाकारों की कहानियों का प्रमुख तत्त्व बन गया। जीवन के सुख-दुख को इन्होंने संदर्भों से उठाकर अपनी कहानियों का विषय बना लिय़ा। जाहिर है कि कहानी की रचना-प्रक्रिया के क्षेत्र में यह एक बड़ा परिवर्तन था और इसने नयी कहानी को सीधे प्रेमचंद से जोड़ दिया। इसका एक कारण यह भी था कि इस दौर के नये लेखकों ने न सिर्फ आजादी की वास्तविकता को स्वीकार किया वरन् स्वाधीन भारत के नये निर्माताओं के सामने देश की वास्तविक तश्वीर प्रस्तुत की। उसे कहीं आशा थी कि शायद आजादी के सच्चे हकदार देश के करोड़ों शोषित-पीड़ित जनों के जीवन में कोई परिवर्तन आयेगा।
गाँवों, कस्बों, छोटे शहरों और अंचलों से आए लेखकों ने इस काल में कथा-वस्तु का अद्भुत विस्तार किया। रेणु का उपन्यास मैला आंचल (1954) और मेरी कहानी संग्रह-पान-फूल (1954) के प्रकाशन के साख लोगों का ध्यान फिर से गाँवों और उससे भी आगे बढ़कर अंचलों की ओर गया। परिवर्तन की गहरी आकांक्षा से जुड़े अनेक लेखकों ने अपने समय की सच्चाइयों का जैसा वास्तविकतावादी चित्र उपस्थित किया वह हिन्दी में प्रेमचंद के बाद पहली बार हुआ था। यही कारण है कि नयी कहानियों के दौर में कहानी साहित्य की केन्द्रीय विधा बना गयी।
आजादी के बाद व्यक्तिगत क्षेत्र में पूँजी का तेजी से जमाव हुआ। पूंजीपतियों ने जमीदारों के सहयोग से धीरे-धीरे सत्ता को अपने वश में कर लिया। 1962 के चीन के हमले के बाद भारतीय अर्थतन्त्र की रीढ़ टेढ़ी हो गयी। निराशा और अवसाद के इस वातावरण में लोगों का स्वर यहाँ तक बदल गया कि वे मुक्ति-संग्राम की बात करने लगे। जनता के सोचने-विचारने के ढंग तक का नियमन करने की शक्ति पूँजीशाहों में आ गयी। संस्कृति के क्षेत्र को इस तरह गंदला कर दिया गया कि भले-बुरे की पहचान लुप्त होने लगी। संघर्षशील मनुष्य की अस्मिता से जुड़ी हुई रचनाशीलता के सामने जीवन-मरण का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। यही कारण था कि साठ के बाद आये लेखकों के सामने रचना की एक अवरुद्ध गली मात्र शेष रह गयी थी, फिर भी उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कथाकारों की भाँति अपने समय की वास्तविकता को ही रचाना का उद्देश्य बनाया।
कुल मिलाकर इस संकलन में जिन संग्रहों को एक साथ प्रकाशित किया जा रहा है, उनके पीछे सांस्कृतिक विकास की वही दृष्टि रही है। इसलिए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि पाठक इस संकलन में एक लंबे दौर की सभी कहानियों को एक साथ पा सकेंगे। परम्परा और विकास को एक साथ समझने में सुविधा होगी।
नयी कहानी का उदय इसी उलझे हुए सामाजिक संदर्भ में स्वाधीनता की सहज मान्यता के कारण, आशा भरे उत्साह के बीच हुआ। शुरू के प्रगतिशील दौर की जनोन्मुखी दृष्टि इसे विरासत में मिली थी। इस काल-खण्ड में नये–नये आने वाले लेखकों ने प्रगतिशील कहानियों की मुख्य कमजोरी को भलीभाँति समझा था। यही कारण था कि उन्हें कि उन्होंने अपनी कथा रचना का मूलाधार वहीं खड़ा किया जिसकी उपेक्षा के कारण व्यक्तिवादी रचनाकार और प्रगतिशाल दोनों फीके पड़ गये थे।
सामाजिक संदर्भों का वास्तविक चित्रण नये कथाकारों की कहानियों का प्रमुख तत्त्व बन गया। जीवन के सुख-दुख को इन्होंने संदर्भों से उठाकर अपनी कहानियों का विषय बना लिय़ा। जाहिर है कि कहानी की रचना-प्रक्रिया के क्षेत्र में यह एक बड़ा परिवर्तन था और इसने नयी कहानी को सीधे प्रेमचंद से जोड़ दिया। इसका एक कारण यह भी था कि इस दौर के नये लेखकों ने न सिर्फ आजादी की वास्तविकता को स्वीकार किया वरन् स्वाधीन भारत के नये निर्माताओं के सामने देश की वास्तविक तश्वीर प्रस्तुत की। उसे कहीं आशा थी कि शायद आजादी के सच्चे हकदार देश के करोड़ों शोषित-पीड़ित जनों के जीवन में कोई परिवर्तन आयेगा।
गाँवों, कस्बों, छोटे शहरों और अंचलों से आए लेखकों ने इस काल में कथा-वस्तु का अद्भुत विस्तार किया। रेणु का उपन्यास मैला आंचल (1954) और मेरी कहानी संग्रह-पान-फूल (1954) के प्रकाशन के साख लोगों का ध्यान फिर से गाँवों और उससे भी आगे बढ़कर अंचलों की ओर गया। परिवर्तन की गहरी आकांक्षा से जुड़े अनेक लेखकों ने अपने समय की सच्चाइयों का जैसा वास्तविकतावादी चित्र उपस्थित किया वह हिन्दी में प्रेमचंद के बाद पहली बार हुआ था। यही कारण है कि नयी कहानियों के दौर में कहानी साहित्य की केन्द्रीय विधा बना गयी।
आजादी के बाद व्यक्तिगत क्षेत्र में पूँजी का तेजी से जमाव हुआ। पूंजीपतियों ने जमीदारों के सहयोग से धीरे-धीरे सत्ता को अपने वश में कर लिया। 1962 के चीन के हमले के बाद भारतीय अर्थतन्त्र की रीढ़ टेढ़ी हो गयी। निराशा और अवसाद के इस वातावरण में लोगों का स्वर यहाँ तक बदल गया कि वे मुक्ति-संग्राम की बात करने लगे। जनता के सोचने-विचारने के ढंग तक का नियमन करने की शक्ति पूँजीशाहों में आ गयी। संस्कृति के क्षेत्र को इस तरह गंदला कर दिया गया कि भले-बुरे की पहचान लुप्त होने लगी। संघर्षशील मनुष्य की अस्मिता से जुड़ी हुई रचनाशीलता के सामने जीवन-मरण का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। यही कारण था कि साठ के बाद आये लेखकों के सामने रचना की एक अवरुद्ध गली मात्र शेष रह गयी थी, फिर भी उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कथाकारों की भाँति अपने समय की वास्तविकता को ही रचाना का उद्देश्य बनाया।
कुल मिलाकर इस संकलन में जिन संग्रहों को एक साथ प्रकाशित किया जा रहा है, उनके पीछे सांस्कृतिक विकास की वही दृष्टि रही है। इसलिए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि पाठक इस संकलन में एक लंबे दौर की सभी कहानियों को एक साथ पा सकेंगे। परम्परा और विकास को एक साथ समझने में सुविधा होगी।
-मार्कण्डेय
गुलरा के बाबा
‘‘कवन है रे वह सरपत काट रहा ?’’
बाबा ने अमिलहवा
के नीचे खड़े होकर अपनी लाठी कंधे से उतारते हुए कहा। आवाज़ सारी गुला में
गूंज गयी। बड़ी गंभीर और बुलंद आवाज़ थी वह; अनजान आदमी तो एक बार डर जाए
और चिरइ-चुरमुन भी पेड़ों पर से उड़ पड़ें। गुलरा की इस आमों की बगिया का
एक-एक जीवन, एक-एक पत्ता बाबा के इस गर्जन से परिचित हैं। क्यों न हों,
बाबा रात-दिन इन्हीं पेड़ों की सेवा-सत्कार में तो लगे रहते हैं।
पर बाबा की पुकार का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक बार नीचे सिर किया और अपने उधरे शरीर को देखा, चमड़े झूल गए थे और उन पर बेशुमार झुर्रियाँ पड़ गयी थीं। पर पचहथे जवान, भींट ऐसी छाती और हाथी की सूँड़ जैसे हाथ, बड़ी-बड़ी तेज़ आंखें; लोग हनुमान कहते थे बाबा को, हनुमान ! मेले-ठेले में अपने पिता गंजन सिंह के लिए रास्ता बनाने का काम बाबा ही करते थे। बड़ी-बड़ी भीड़ को पानी की काई की तरह इधर-उधर कर देना उनके लिए कोई विशेष बात न थी। बखरी में खाने घुसते समय बिटियों-पतोहुओं को जता देना तो जरूरी होता न ! बाबा दालान ही में से खाँसते और सारी बखरियों के कुत्ते मारे डर के भाग के बाहर हो जाते।
बाबा के दिल को धक्का लगा। वे गुलरा के बाबा कहे जाते हैं; इतना बड़ा जंगल और बाग उनके ही ऊपर छोड़ रक्खा है परिवार वालों ने, और यहाँ दस कोस में कौन नहीं जानता इसे...उनका आहत अभिमान नयी भाषा में बोला-बुढ़ापे के एहसास के कारण-और क्रोध की हल्की गर्मी उनके शरीर में दौड़ गयी। उन्होंने बगल में देखा, लेहसुनवाँ में नये गोंफे आ गये थे, शायद इस साल इसमें बौर भी आ जाएँ, और फिर धीरे-धीरे उस हिलती सरपत की ओर चल पड़े।
चैतू अहीर था—पूरा चेलिक; करीब चौबीस-पचीस का, काला मजीठ शरीर, जैसे कोल्हू की जाट। इसी ने तो बनारस के मशहूर पहलवान झग्गा को पटक दिया-केवल दो ही मिनट में।
चैतू बाबा को देख कर रुक गया।
‘‘सलाम ठाकुर !’’
‘‘खुश रहो चैतू; लेकिन तुम यह क्या कर रहे हो ?’’
‘‘सरपत काट रहे हैं ठाकुर !’’
‘‘अच्छा कल से मत काटना !’’
‘‘ऐसे ही काटूँगा।’’ और चैतू लटक कर हँसिया चलाने लगा।
‘‘यह बात नहीं चैतू !’’ बाबा सागर की-सी गहराई से कहते गये, ‘‘मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। अपने दो-एक संगी साथियों और बूढ़-पुरानियों को भी बुलाये आना—यहीं; यदि तुम मेरा गट्ठा टेढ़ा कर दोगे, तो मैं कभी जबान नहीं खोलूँगा और यदि नहीं, तो तुम कल से यहाँ दिखाई न पड़ना ?’’
चैतू कटी-कटाई सरपत छोड़ कर चला गया। दूसरे दिन बाबा सभी भाई, कुछ गाँव के तमाशबीन और चैतू के अपने संगी-साथी; खासी भीड़ हो गयी थी। बाबा ने बाँह फैला दी—बीते भर नीचे तक झुर्रीदार चमड़ा लटक गया और चैतू ने दाँत पीस-पीस कर जोर लगाया—माथे पर पसीना हो आया, पर बाबा का हाथ टस-से-मस न हुआ।
किसी ने कहा, ‘‘बस चैतू, अब तुम अपना हाथ फैलाव !’’ चैतू ने हाथ फैलाया और बाबा ने बच्चे की तरह उसे मरोड़ कर दबा दिया। चैतू चिचिया उठा। बाबा ने छोड़ दिया।
बाबा के छोटे भाई देवी सिंह लठैत थे। उनसे चैतू की यह धृष्टता देखी नहीं जा रही थी, पर बाबा ने कहा, ‘‘ऐसा मत करो।’’ और अब, जब वह हार गया, तो वे एकाएक उबल पड़े, ‘‘कहो तो दे दूँ दो बाँस साले की पीठ पर !’’ बाबा ने देवी सिंह को डाँटा। वे सिटपिटा गये। चारों ओर बाबा के पौरुष की तारीफें होने लगीं, पर वे जैसे उदास हो गये थे।
फागुन के दूसरे पखवारे के थोड़े ही दिन बाकी थे—दिन को सुनहली धूप, शाम को अबीरी आकाश और रात को रुपहली, टहकी चाँदनी—खलिहान जौ-गेहूँ के डाँठ से खचा-खच भरे हुए। हवा भी चिबोला करती हैं न ! बकरिदिया ठाकुर के घर में नहा कर लौट रही थी—फगुनहट का झोंका आया और आँचल उड़ा कर चला गया—‘‘शरमा गयी बकरीदा ! इसमें क्या बात है जी, फागुन में बाबा देवर लागें !’’ देवकी पंडित ने आज खूब छान ली थी !
‘‘भौजी मेरी सिलिक की कमीज रद्द कर दी।’’ नन्हकुआ मुस्कराता जा रहा था और हाथ से कमीज खुजा रहा था।
‘‘जीताबो आज खूब फँसी। बड़ी उस्ताद बनती थी न ! आज पड़ गया सुधुआ से पाला, कलाई मरोड़ कर रंग का लोटा छीन लिया और खूब नहला कर गालों पर ऐसी रोली मली की बच्ची को छट्ठी का दूध याद आ गया।’’
पर बाबा की पुकार का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक बार नीचे सिर किया और अपने उधरे शरीर को देखा, चमड़े झूल गए थे और उन पर बेशुमार झुर्रियाँ पड़ गयी थीं। पर पचहथे जवान, भींट ऐसी छाती और हाथी की सूँड़ जैसे हाथ, बड़ी-बड़ी तेज़ आंखें; लोग हनुमान कहते थे बाबा को, हनुमान ! मेले-ठेले में अपने पिता गंजन सिंह के लिए रास्ता बनाने का काम बाबा ही करते थे। बड़ी-बड़ी भीड़ को पानी की काई की तरह इधर-उधर कर देना उनके लिए कोई विशेष बात न थी। बखरी में खाने घुसते समय बिटियों-पतोहुओं को जता देना तो जरूरी होता न ! बाबा दालान ही में से खाँसते और सारी बखरियों के कुत्ते मारे डर के भाग के बाहर हो जाते।
बाबा के दिल को धक्का लगा। वे गुलरा के बाबा कहे जाते हैं; इतना बड़ा जंगल और बाग उनके ही ऊपर छोड़ रक्खा है परिवार वालों ने, और यहाँ दस कोस में कौन नहीं जानता इसे...उनका आहत अभिमान नयी भाषा में बोला-बुढ़ापे के एहसास के कारण-और क्रोध की हल्की गर्मी उनके शरीर में दौड़ गयी। उन्होंने बगल में देखा, लेहसुनवाँ में नये गोंफे आ गये थे, शायद इस साल इसमें बौर भी आ जाएँ, और फिर धीरे-धीरे उस हिलती सरपत की ओर चल पड़े।
चैतू अहीर था—पूरा चेलिक; करीब चौबीस-पचीस का, काला मजीठ शरीर, जैसे कोल्हू की जाट। इसी ने तो बनारस के मशहूर पहलवान झग्गा को पटक दिया-केवल दो ही मिनट में।
चैतू बाबा को देख कर रुक गया।
‘‘सलाम ठाकुर !’’
‘‘खुश रहो चैतू; लेकिन तुम यह क्या कर रहे हो ?’’
‘‘सरपत काट रहे हैं ठाकुर !’’
‘‘अच्छा कल से मत काटना !’’
‘‘ऐसे ही काटूँगा।’’ और चैतू लटक कर हँसिया चलाने लगा।
‘‘यह बात नहीं चैतू !’’ बाबा सागर की-सी गहराई से कहते गये, ‘‘मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। अपने दो-एक संगी साथियों और बूढ़-पुरानियों को भी बुलाये आना—यहीं; यदि तुम मेरा गट्ठा टेढ़ा कर दोगे, तो मैं कभी जबान नहीं खोलूँगा और यदि नहीं, तो तुम कल से यहाँ दिखाई न पड़ना ?’’
चैतू कटी-कटाई सरपत छोड़ कर चला गया। दूसरे दिन बाबा सभी भाई, कुछ गाँव के तमाशबीन और चैतू के अपने संगी-साथी; खासी भीड़ हो गयी थी। बाबा ने बाँह फैला दी—बीते भर नीचे तक झुर्रीदार चमड़ा लटक गया और चैतू ने दाँत पीस-पीस कर जोर लगाया—माथे पर पसीना हो आया, पर बाबा का हाथ टस-से-मस न हुआ।
किसी ने कहा, ‘‘बस चैतू, अब तुम अपना हाथ फैलाव !’’ चैतू ने हाथ फैलाया और बाबा ने बच्चे की तरह उसे मरोड़ कर दबा दिया। चैतू चिचिया उठा। बाबा ने छोड़ दिया।
बाबा के छोटे भाई देवी सिंह लठैत थे। उनसे चैतू की यह धृष्टता देखी नहीं जा रही थी, पर बाबा ने कहा, ‘‘ऐसा मत करो।’’ और अब, जब वह हार गया, तो वे एकाएक उबल पड़े, ‘‘कहो तो दे दूँ दो बाँस साले की पीठ पर !’’ बाबा ने देवी सिंह को डाँटा। वे सिटपिटा गये। चारों ओर बाबा के पौरुष की तारीफें होने लगीं, पर वे जैसे उदास हो गये थे।
फागुन के दूसरे पखवारे के थोड़े ही दिन बाकी थे—दिन को सुनहली धूप, शाम को अबीरी आकाश और रात को रुपहली, टहकी चाँदनी—खलिहान जौ-गेहूँ के डाँठ से खचा-खच भरे हुए। हवा भी चिबोला करती हैं न ! बकरिदिया ठाकुर के घर में नहा कर लौट रही थी—फगुनहट का झोंका आया और आँचल उड़ा कर चला गया—‘‘शरमा गयी बकरीदा ! इसमें क्या बात है जी, फागुन में बाबा देवर लागें !’’ देवकी पंडित ने आज खूब छान ली थी !
‘‘भौजी मेरी सिलिक की कमीज रद्द कर दी।’’ नन्हकुआ मुस्कराता जा रहा था और हाथ से कमीज खुजा रहा था।
‘‘जीताबो आज खूब फँसी। बड़ी उस्ताद बनती थी न ! आज पड़ गया सुधुआ से पाला, कलाई मरोड़ कर रंग का लोटा छीन लिया और खूब नहला कर गालों पर ऐसी रोली मली की बच्ची को छट्ठी का दूध याद आ गया।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i