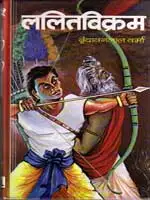|
नाटक-एकाँकी >> ललितविक्रम ललितविक्रमवृंदावनलाल वर्मा
|
347 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है उत्कृष्ट नाटक....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
इस पुस्तक में इतिहास के सुंदर अतीत की एक एक गाथा को उसके अनुरूप वातावरण
में सफलतापूर्वक उपस्थित किया है। राजा, सभा, आश्रम, गुरु, शिष्य सभी के
चित्रण में नाटककार की कल्पना संतुलित तथ्यनिष्ठ रही हैं, जिससे हमें युग
विशेष की परिस्थितियाँ विकास की दिशा और पथ की बाधाएँ अपरिचित नहीं जान
पड़तीं।
दो शब्द
हमारा भविष्य जैसे कल्पना के परे दूर तक फैला हुआ है, हमारा अतीत भी उसी
प्रकार स्मृति के पार तक विस्तृत है। अतीत के जिस अंश तक प्रमाण की किरणें
पहुँच सकती हैं उसे हम इतिहास की संज्ञा देते हैं जो जीतने के स्पंदन से
रहित इतिवृत्त मात्र है। जो हमारे तर्क की सीमा के पार घटित हो चुका है,
वह पुराण की सीमा में आबद्ध होकर जीवन की ऐसी गाथा बन जाता है, जिसमें
इतिवृत्त का सूत्र खोजना कठिन है। हर युग की अनुश्रुति पुराण पर कल्पना का
नया रंग चढ़ा देती है और इस प्रकार हम तक आते- आते यह जीवन गाथा सत्य,
कल्पना सिद्धांत आदर्श नीति आदि का संघात बन जाती है।
इतिहास को साहित्य में प्रतिष्ठित करने के लिए घटना को जीवन से और जीवन को मनुष्य के मनोरागों से जोड़ना पड़ता है। परंतु पुराण तो स्वयं विराट् साहित्य का अंश है। अतः उसकी बुद्धिसम्मत भागवत व्याख्या ही उसे हमारे जीवन के निकट ला सकती है। यह कार्य सहज नहीं, क्योंकि एक ओर अनुभूति की न्यूनता इस, व्याख्या को नीरस सिद्धांत बना सकती है और दूसरी ओर अनुभूति की अधिकता में वह विश्वसनीय नहीं रहती।
इतिहास, के अन्यतम जीवन-शिल्पी श्री वृंदावनलालजी ने सुंदर अतीत की एक-एक गाथा को उसके अनुरूप वातावरण में सफलतापूर्वक उपस्थित किया है। राजा, सभा, आश्रम, गुरु, शिष्य सभी के चित्रण में नाटककार की कल्पना संतुलित तथ्यनिष्ठ रही है; जिससे हमें युग विशेष की परिस्थितियाँ विकास की दिशा और पथ की बाधाएँ अपरिचित नहीं जान पड़ती।
हमारी संस्कृति-प्रवाहिनी ऊपर से सम और शांत है, परंतु उसके तल में अनेक ज्वालामुखियाँ जली बुझी हैं, असंख्य तूफान जागे सोए हैं। दर्शन धर्म साहित्य नीति कर्म आदि सभी क्षेत्रों में विद्रोहियों की स्थिति रही है; पर तोड़ने वाले हथौड़े को मूर्तिकार की छेनी बना लेने की विशेषता हमारी अपनी है। इसी कारण विद्रोह ने हमारी जीवन प्रतिभा को पूर्णता दी है, उसे विकलांग नहीं किया।
विद्रोही धौम्य ऋषि भावी पीढ़ी के शिल्पी हैं और विद्रोही रोमक वर्तमान के। उन दोनों के विद्रोह ने तत्कालीन रुद्ध जीवन को प्रशस्त क्षितिज देकर सफलता प्राप्त की।
नाटक में भारतीय जीवन की मूलभूत विशेषताएँ सुरक्षित रह सकी हैं, इसका श्रेय नाटककार की सूक्ष्म पर लक्ष्यबद्ध दृष्टि को दिया जाएगा।
‘कृत संपद्यते चरन्’ का महामंत्र नाटक में बार-बार गूँजता है।
इतिहास को साहित्य में प्रतिष्ठित करने के लिए घटना को जीवन से और जीवन को मनुष्य के मनोरागों से जोड़ना पड़ता है। परंतु पुराण तो स्वयं विराट् साहित्य का अंश है। अतः उसकी बुद्धिसम्मत भागवत व्याख्या ही उसे हमारे जीवन के निकट ला सकती है। यह कार्य सहज नहीं, क्योंकि एक ओर अनुभूति की न्यूनता इस, व्याख्या को नीरस सिद्धांत बना सकती है और दूसरी ओर अनुभूति की अधिकता में वह विश्वसनीय नहीं रहती।
इतिहास, के अन्यतम जीवन-शिल्पी श्री वृंदावनलालजी ने सुंदर अतीत की एक-एक गाथा को उसके अनुरूप वातावरण में सफलतापूर्वक उपस्थित किया है। राजा, सभा, आश्रम, गुरु, शिष्य सभी के चित्रण में नाटककार की कल्पना संतुलित तथ्यनिष्ठ रही है; जिससे हमें युग विशेष की परिस्थितियाँ विकास की दिशा और पथ की बाधाएँ अपरिचित नहीं जान पड़ती।
हमारी संस्कृति-प्रवाहिनी ऊपर से सम और शांत है, परंतु उसके तल में अनेक ज्वालामुखियाँ जली बुझी हैं, असंख्य तूफान जागे सोए हैं। दर्शन धर्म साहित्य नीति कर्म आदि सभी क्षेत्रों में विद्रोहियों की स्थिति रही है; पर तोड़ने वाले हथौड़े को मूर्तिकार की छेनी बना लेने की विशेषता हमारी अपनी है। इसी कारण विद्रोह ने हमारी जीवन प्रतिभा को पूर्णता दी है, उसे विकलांग नहीं किया।
विद्रोही धौम्य ऋषि भावी पीढ़ी के शिल्पी हैं और विद्रोही रोमक वर्तमान के। उन दोनों के विद्रोह ने तत्कालीन रुद्ध जीवन को प्रशस्त क्षितिज देकर सफलता प्राप्त की।
नाटक में भारतीय जीवन की मूलभूत विशेषताएँ सुरक्षित रह सकी हैं, इसका श्रेय नाटककार की सूक्ष्म पर लक्ष्यबद्ध दृष्टि को दिया जाएगा।
‘कृत संपद्यते चरन्’ का महामंत्र नाटक में बार-बार गूँजता है।
महादेवी वर्मा
परिचय
वैदिक काल के एक अंग पर कुछ लिखने की बहुत समय से इच्छा थी। उस काल की
तरुण और सद्यः ओजस्विता का स्पंदन इतिहास और कथाओं में स्थान-स्थान पर
मिलता है। विकास का क्रम अनंत है और मानव की वह ओजस्विता भी। किसी-किसी
युग में विकास-क्रम में कुछ कड़ियाँ सड़ी-गली और निर्बल भी दिखलाई पड़ती
हैं-हमारे ही देश में नहीं, पृथ्वी के अन्य भागों में भी। इनके होते हुए
भी मानव विकास मार्ग पर अग्रसर होता रहता है, भले ही समीचीन रूप से वह
दिखलाई न पड़े। मानव संपूर्णतया कभी अशक्त नहीं होता, हो नहीं सकता-यदि
ऐसा हो तो सृष्टि का कार्य खंडित हो जाए। हमें अपने समाज में जो कुछ भी
शिथिलता अकर्मण्यता और ऊँचे आदर्श के प्रति गतिहीनता दिखलाई पड़ती है वह
विकास के क्रम की एक कड़ी मात्र है, जो चिरकाल तक नहीं रह सकती। प्रश्न जो
ऐसी परिस्थिति में उठता है वह है-कब तक यह अवस्था चलेगी ? कब तक इसे रहने
दिया जावे अथवा सहन किया जावे ? जैसे ही उसके उत्तर की बात सोची जाती है,
प्रश्न समस्या का रूप धारण कर लेता है। प्रगति की बात सोचते ही समस्या के
सुलझाव को तत्काल गति देने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है।
अनेक लोग प्रायः और संध्या संकल्प करते हैं कि हम सौ वर्ष जिएँ, सौ शरद् ऋतुएँ देखें, सौ वर्ष तक बोलते और कार्य करते रहें इत्यादि। परंतु कैसे ? दूसरों का शोषण करके ? मनमाने भोग-विलासों के संसर्ग में रहते हुए ? जब तक जीवन में संयम और रहन-सहन में अनुशासन न बरता जाए, यह संभव नहीं। वैसी चाह का बना रहना नैसर्गिक है, परंतु इस कामना के मन में बसे रहने मात्र से होता ही क्या है !
प्राचीन काल में संयम और अनुशासन की परिपाटी का विवेक के साथ अनुशीलन किया जाता था। उद्देश्य में अस्पष्टता नहीं थी, मन में भ्रम को बसने नहीं दिया जाता था। कार्य विधि में दृढ़ संकल्प से काम लिया जाता था। इसलिए जीवन की विविध झाँकियों में ओज की सद्यता और तरुणता दिखलाई पड़ती है।
आर्थिक कठिनाइयाँ प्रत्येक युग में मानव को संतप्त करने के लिए खड़ी हो हो जाती हैं और वह उनका सामना करता है। आर्थिक कठिनाइयों के अतिरिक्त मानसिक और आध्यात्मिक उलझनें भी मनुष्य को दुर्बल बनाने में कसर नही लगातीं। आर्थिर क्लेशों के साथ जब ये भी लग जाती हैं तब तो कष्टों की दुःसहता बहुत बढ़ जाती है। इन सबके होते हुए मनुष्य कैसे कामना करे कि मैं बल पराक्रम से संयुक्त रहकर सौ सुहावनी शरदों को देखता रहूँ ? अपनी कठिनाई स्पष्ट समझ में आ जावे और मति विभ्रम न हो तो दृढ़ संकल्प के आश्रय से मनुष्य अवश्य आगे बढ़ सकता है। प्रकृति की क्रियाओं में आतंक और सलोनापन दोनों हैं। मानव उस आतंक से भयभीत न होकर प्रकृति के सलोनेपन में से अपने मन के लिए शक्ति और पुरुषार्थ को खींचे तो वह निस्संदेह अपनी उस स्वच्छ कामना को सफल कर सकता है, जो उस प्रार्थना में व्याप्त है-‘मैं सो-सौ शरद् ऋतुओं को अदीन होकर देखता रहूँ।"
समाज में जब विभ्रम और भय का घुन लग जाता है, आस्था निर्बल हो जाती है, संकल्प चंचल हो उठता है, पर-शोषण बढ़ जाता है, अहंकार, दंभ और अनृत के हठ की बाढ़ आ जाती है तब विकास क्रम की कड़ी गलत दिखलाई पड़ने लगती है।
फिर भी मानव रटता रहता है-मैं सौ बरस तक जीवित रहूँ। सो कैसे ? विकास-क्रम का नियम केवल रट को कभी सफल नहीं होने देगा। इस संकल्प को और भी कई तत्त्वों की संगति चाहिए। उनमें बुद्धि और विवेक का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है।
जिस काल में इस शिव संकल्प को बुद्धि और विवेक का सहयोग प्राप्त रहा होगा उस काल में भी मानव के सामने कठिनाइयों और बाधाओं के पहाड़ आ खड़े होते होंगे और वह उनका सफलता के साथ प्रतिरोध करता होगा। प्राचीन के इतिहास और साहित्य में इस तथ्य के उदाहरण सुने थे। सोचा, कुछ अधिक हस्तगत करने का प्रयत्न करूँ।
एक दिन इसी उधेडबुन में था कि अपनी छोटी सी बालिका को एक पुस्तक में पढ़ते हुए सुना-अयोध्या के एक राजा थे। बहुत अकाल पड़े। प्रजा दुःखी हो गई। राजा को किसी ऋषि ने बतलाया कि तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसलिए अकाल पर अकाल पड़ रहे हैं; उसे मार दो तो अकाल का युग समाप्त हो जावेगा। राजा ने कहा, मैं राज्य छोड़ने को तैयार हूँ, परंतु यह दुकर्म करने को तैयार नहीं। इस पर ऋषि ने कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था।
इस कहानी ने अनेक सुझाव दिए और मैं उसके मूल स्रोत की ओर आकृष्ट हुआ।
डॉ. नारायणचंद्र वंद्योपाध्याय की पुस्तक Economic life and progress in Ancient India" पृष्ठ 325 पर रोमपाद नाम के अयोध्या नरेश के राज्यकाल में भयानक अकाल पड़ने का वृत्तांत मिला। अकाल का विस्तृत ब्योरा। वाल्मीकि रामायण में है। रोमपाद को मैंने अपने नाटक में रोमक कर दिया है, क्योंकि अयोध्या नरेशों की एक वंशावलि में रोमपाद नाम नहीं आया है, रोमक आया है और मुझे यही नाम अच्छा लगा। रोमक के पुत्र का नाम कुछ और था, परंतु मैंने उसके सुंदर और कल्याणकारी पराक्रम के कारण उसका नाम ललितविक्रम रख दिया है। उसी के नाम पर यह नाटक है।
उत्तरवैदिक काल में दासता का एक रूप समाज में प्रचलित था। द्विज तक दास हो जाते थे। ऋण न चुका पाने पर स्वतंत्र जन को दास हो जाना पड़ता था। दासोद्धार के उपाय भी थे (डॉ. वंद्योपाध्याय की वही पुस्तक, पृष्ठ 295-98)।
उत्तर वैदिक काल में पणि (फिनीशियन) आर्यावर्त में व्यापार करते थे। उनके बड़े-बड़े पोत चलते थे। वे ब्याजभोजी थे। संभव है, आज का ‘बनिया’ शब्द वणिक का अपभ्रंश न होकर पणि का ही रूपांतर हो। दास बनाने वाले ब्याजभोजियों के प्रति आर्यों की घृणा स्वाभाविक थी। आर्य वणिक कृषि और वणिज्य करते थे, पणियों का प्रधान व्यवसाय व्यापार और लेन-देन था।
तत्कालीन समाज का स्थिति-चित्रण इस नाटक में करने की चेष्टा की गई है। राजा ने अखंड और अनियंत्रित सत्ताधारी का रूप नहीं कर पाया था। गौतम धर्मसूत्र के एकादश अध्याय में-‘राजा सर्वस्येष्टो ब्राह्मण वर्जम्’ ब्राह्मण को छोड़ राजा सबका अधिपति है’-पीछे की बात है। उत्तरवैदिक काल में राजा को चुनने और निकाल देने तथा फिर चुन लेने का अधिकार समिति को था-‘ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह’ तथा नाऽस्मै कल्पते’ (Dr. Radha Kumud Mukurji’s Hinhu Civilisation p, 99 and p. 100) अथर्ववेद 3:3:5;6:88;5:19)। समिति का सभापति ‘ईशान’ कहलाता था। चुनाव की प्रथा वही थी जो नाटक में दी गई है। राजा के पदच्युत किए जाने या एक नियत समय के लिए निकाल देने की प्रथा भी थी; जिसका वर्णन नाटक में आया है। देश के प्रति जनता में गाढ़ा प्रेम था। उसकी प्रतिध्वनि मनुस्मृति और श्रीमद्भागवत में ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वगादपि गरीयसी’ की सूक्ति में आई है। ऋग्वेद में ‘स्वराज्य’ शब्द स्पष्ट रूप से आया है-‘यतेमहि स्वराज्ये’ (5:66:6)-हम स्वराज्य के लिए प्रयत्नशील रहें। यह वह युग था जब साधारण आर्यजन का मन घोर विपत्तियों और कठिनाइयों के सामने न तो झुकता था और न थकता था-तरुण, तेजस्वी और सदा ओज से भरा हुआ। वे एक-दूसरे से कहते थे-‘उद्बबुध्वं समनसः सखाय’ (ऋग्वेद 10: 101: 1: )
अनेक लोग प्रायः और संध्या संकल्प करते हैं कि हम सौ वर्ष जिएँ, सौ शरद् ऋतुएँ देखें, सौ वर्ष तक बोलते और कार्य करते रहें इत्यादि। परंतु कैसे ? दूसरों का शोषण करके ? मनमाने भोग-विलासों के संसर्ग में रहते हुए ? जब तक जीवन में संयम और रहन-सहन में अनुशासन न बरता जाए, यह संभव नहीं। वैसी चाह का बना रहना नैसर्गिक है, परंतु इस कामना के मन में बसे रहने मात्र से होता ही क्या है !
प्राचीन काल में संयम और अनुशासन की परिपाटी का विवेक के साथ अनुशीलन किया जाता था। उद्देश्य में अस्पष्टता नहीं थी, मन में भ्रम को बसने नहीं दिया जाता था। कार्य विधि में दृढ़ संकल्प से काम लिया जाता था। इसलिए जीवन की विविध झाँकियों में ओज की सद्यता और तरुणता दिखलाई पड़ती है।
आर्थिक कठिनाइयाँ प्रत्येक युग में मानव को संतप्त करने के लिए खड़ी हो हो जाती हैं और वह उनका सामना करता है। आर्थिक कठिनाइयों के अतिरिक्त मानसिक और आध्यात्मिक उलझनें भी मनुष्य को दुर्बल बनाने में कसर नही लगातीं। आर्थिर क्लेशों के साथ जब ये भी लग जाती हैं तब तो कष्टों की दुःसहता बहुत बढ़ जाती है। इन सबके होते हुए मनुष्य कैसे कामना करे कि मैं बल पराक्रम से संयुक्त रहकर सौ सुहावनी शरदों को देखता रहूँ ? अपनी कठिनाई स्पष्ट समझ में आ जावे और मति विभ्रम न हो तो दृढ़ संकल्प के आश्रय से मनुष्य अवश्य आगे बढ़ सकता है। प्रकृति की क्रियाओं में आतंक और सलोनापन दोनों हैं। मानव उस आतंक से भयभीत न होकर प्रकृति के सलोनेपन में से अपने मन के लिए शक्ति और पुरुषार्थ को खींचे तो वह निस्संदेह अपनी उस स्वच्छ कामना को सफल कर सकता है, जो उस प्रार्थना में व्याप्त है-‘मैं सो-सौ शरद् ऋतुओं को अदीन होकर देखता रहूँ।"
समाज में जब विभ्रम और भय का घुन लग जाता है, आस्था निर्बल हो जाती है, संकल्प चंचल हो उठता है, पर-शोषण बढ़ जाता है, अहंकार, दंभ और अनृत के हठ की बाढ़ आ जाती है तब विकास क्रम की कड़ी गलत दिखलाई पड़ने लगती है।
फिर भी मानव रटता रहता है-मैं सौ बरस तक जीवित रहूँ। सो कैसे ? विकास-क्रम का नियम केवल रट को कभी सफल नहीं होने देगा। इस संकल्प को और भी कई तत्त्वों की संगति चाहिए। उनमें बुद्धि और विवेक का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है।
जिस काल में इस शिव संकल्प को बुद्धि और विवेक का सहयोग प्राप्त रहा होगा उस काल में भी मानव के सामने कठिनाइयों और बाधाओं के पहाड़ आ खड़े होते होंगे और वह उनका सफलता के साथ प्रतिरोध करता होगा। प्राचीन के इतिहास और साहित्य में इस तथ्य के उदाहरण सुने थे। सोचा, कुछ अधिक हस्तगत करने का प्रयत्न करूँ।
एक दिन इसी उधेडबुन में था कि अपनी छोटी सी बालिका को एक पुस्तक में पढ़ते हुए सुना-अयोध्या के एक राजा थे। बहुत अकाल पड़े। प्रजा दुःखी हो गई। राजा को किसी ऋषि ने बतलाया कि तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसलिए अकाल पर अकाल पड़ रहे हैं; उसे मार दो तो अकाल का युग समाप्त हो जावेगा। राजा ने कहा, मैं राज्य छोड़ने को तैयार हूँ, परंतु यह दुकर्म करने को तैयार नहीं। इस पर ऋषि ने कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था।
इस कहानी ने अनेक सुझाव दिए और मैं उसके मूल स्रोत की ओर आकृष्ट हुआ।
डॉ. नारायणचंद्र वंद्योपाध्याय की पुस्तक Economic life and progress in Ancient India" पृष्ठ 325 पर रोमपाद नाम के अयोध्या नरेश के राज्यकाल में भयानक अकाल पड़ने का वृत्तांत मिला। अकाल का विस्तृत ब्योरा। वाल्मीकि रामायण में है। रोमपाद को मैंने अपने नाटक में रोमक कर दिया है, क्योंकि अयोध्या नरेशों की एक वंशावलि में रोमपाद नाम नहीं आया है, रोमक आया है और मुझे यही नाम अच्छा लगा। रोमक के पुत्र का नाम कुछ और था, परंतु मैंने उसके सुंदर और कल्याणकारी पराक्रम के कारण उसका नाम ललितविक्रम रख दिया है। उसी के नाम पर यह नाटक है।
उत्तरवैदिक काल में दासता का एक रूप समाज में प्रचलित था। द्विज तक दास हो जाते थे। ऋण न चुका पाने पर स्वतंत्र जन को दास हो जाना पड़ता था। दासोद्धार के उपाय भी थे (डॉ. वंद्योपाध्याय की वही पुस्तक, पृष्ठ 295-98)।
उत्तर वैदिक काल में पणि (फिनीशियन) आर्यावर्त में व्यापार करते थे। उनके बड़े-बड़े पोत चलते थे। वे ब्याजभोजी थे। संभव है, आज का ‘बनिया’ शब्द वणिक का अपभ्रंश न होकर पणि का ही रूपांतर हो। दास बनाने वाले ब्याजभोजियों के प्रति आर्यों की घृणा स्वाभाविक थी। आर्य वणिक कृषि और वणिज्य करते थे, पणियों का प्रधान व्यवसाय व्यापार और लेन-देन था।
तत्कालीन समाज का स्थिति-चित्रण इस नाटक में करने की चेष्टा की गई है। राजा ने अखंड और अनियंत्रित सत्ताधारी का रूप नहीं कर पाया था। गौतम धर्मसूत्र के एकादश अध्याय में-‘राजा सर्वस्येष्टो ब्राह्मण वर्जम्’ ब्राह्मण को छोड़ राजा सबका अधिपति है’-पीछे की बात है। उत्तरवैदिक काल में राजा को चुनने और निकाल देने तथा फिर चुन लेने का अधिकार समिति को था-‘ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह’ तथा नाऽस्मै कल्पते’ (Dr. Radha Kumud Mukurji’s Hinhu Civilisation p, 99 and p. 100) अथर्ववेद 3:3:5;6:88;5:19)। समिति का सभापति ‘ईशान’ कहलाता था। चुनाव की प्रथा वही थी जो नाटक में दी गई है। राजा के पदच्युत किए जाने या एक नियत समय के लिए निकाल देने की प्रथा भी थी; जिसका वर्णन नाटक में आया है। देश के प्रति जनता में गाढ़ा प्रेम था। उसकी प्रतिध्वनि मनुस्मृति और श्रीमद्भागवत में ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वगादपि गरीयसी’ की सूक्ति में आई है। ऋग्वेद में ‘स्वराज्य’ शब्द स्पष्ट रूप से आया है-‘यतेमहि स्वराज्ये’ (5:66:6)-हम स्वराज्य के लिए प्रयत्नशील रहें। यह वह युग था जब साधारण आर्यजन का मन घोर विपत्तियों और कठिनाइयों के सामने न तो झुकता था और न थकता था-तरुण, तेजस्वी और सदा ओज से भरा हुआ। वे एक-दूसरे से कहते थे-‘उद्बबुध्वं समनसः सखाय’ (ऋग्वेद 10: 101: 1: )
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i