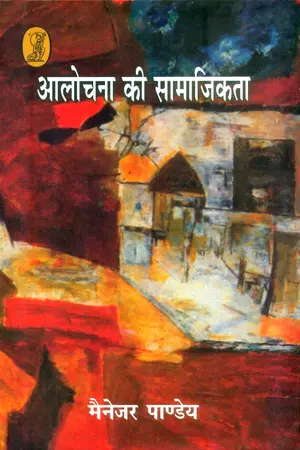|
आलोचना >> आलोचना की सामाजिकता आलोचना की सामाजिकतामैनेजर पाण्डेय
|
|
|||||||
मैनेजर पाण्डेय हिन्दी के शीर्षस्थ मार्क्सवादी आलोचक हैं। पिछले लगभग साढ़े तीन दशकों में तमाम राजनीतिक और वैचारिक उथल-पुथल के बीच भी उनमें किसी प्रकार का वैचारिक और सैद्धान्तिक विचलन नहीं दिखा। सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने कभी भी लोकप्रिय नुस्खे नहीं अपनाए। आज हिन्दी आलोचना में उनकी उपस्थिति उन सभी लोगों के लिए एक भरोसे का विषय है, जो आलोचना के लोकतंत्र में विश्वास रखने के साथ-साथ उससे गहरी सामाजिक सम्बद्धता की माँग करते रहे हैं। मैनेजर पाण्डेय का अब तक का पूरा लेखन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने सामाजिकता के जिस प्रश्न को रचनात्मक साहित्य के मूल्यांकन का प्रमुख आधार बनाया है, उसी प्रश्न को आलोचना और चिन्तन के मूल्यांकन का आधार बनाने से वे कभी नहीं चूके हैं। उनका लेखन एक ऐसे तेजस्वी चिन्तक का लेखन है, जो किसी रचना के रूप पक्ष से ही अघा नहीं जाता, बल्कि रचना के रेशे-रेशे में कौन से विचार हैं, इसकी सूक्ष्म पड़ताल करता है। पूर्व में रामचन्द्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा तथा इस पुस्तक में नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि का मूल्यांकन करते हुए भी उनकी यही मूल्यांकन-दृष्टि कार्य करती रही है। पाण्डेय जी के मूल्यांकन की एक और विशेषता है-अन्ध समर्थक होने से बचना। रचनाकार अथवा चिन्तक-आलोचक चाहे जितना यशस्वी ओर मेधावी हो, पाण्डेय जी बिना किसी भय के अपने आलोचनात्मक औजारों के साथ उसकी रचना या आलोचना संसार में प्रवेश करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि वे आलोच्य रचनाकार अथवा आलोचक के विषय में किसी भी प्रकार के पूर्व निष्कर्षो से बिना प्रभावित हुए गहन संवाद स्थापित करते हैं। यदि आज हिन्दी भाषी समाज के साथ-साथ गैर हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के अध्येता भी पाण्डेय जी के लिखे निबन्धों को बहुत गम्भीरता से पढ़ते-गुनते हैं तो इसके पीछे उनकी अपनी आलोचना की सामाजिकता ही है। समाज से कट कर जिस प्रकार रचनाएँ अर्थहीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार आलोचना भी। यहाँ यह याद आना स्वाभाविक है कि दलित चेतना और स्त्री चेतना की बातें उन्होंने तब की थीं, जब लोगों का ध्यान इस ओर लगभग नहीं के बराबर था।
‘शब्द और कर्म’, ’भक्ति आन्दोलन और सूरदास का काव्य’, ‘साहित्य और इतिहास-दृष्टि’, ‘साहित्य के समाज-शास्त्र की भूमिका’ और ‘अनभै’साँचा’ के बाद इस नयी आलोचना पुस्तक में भी मैनेजर पाण्डेय ने रचना और आलोचना के लिए सामाजिकता को निकष बनाया है। पुस्तक के पहले खण्ड ‘आलोचना का समाज’ में उन्होंने आलोचना की सामाजिकता के साथ ही उसकी राजनीति, उसकी सार्थकता-निरर्थकता पर विचार किया है। यहाँ यह कहना होगा कि इतनी गहरी संलग्नता और वैचारिकता के साथ इन विषयों पर हिन्दी में इसके पहले शायद ही कोई कार्य हुआ हो। अपनीं पुस्तक में पाण्डेय जी जहाँ एक ओर लोकप्रिय साहित्य और मार्क्सवाद के रिश्तों पर जिरह करते हैं, वहीं वे साहित्य के समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पर भी बात करते हैं। पाठकों को याद आ सकता है कि अपनी पुस्तक साहित्य के समाज-शास्त्र की भूमिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी में साहित्य के समाजशास्त्र की एक पुख्ता नींव रखी थी। दुनिया के बड़े विचारकों की तरह मैनेजर पाण्डेय के चिन्तन की विशेषता रही है कि वे साहित्येतर विषयों पर भी गम्भीरता से विचार करते रहे हैं। इस पुस्तक में भी ‘राजनीति की भाषा’, ‘भाषा की राजनीति’ और ‘भाषा की रात में मनुष्य’ जैसे विचारोत्तेजक और मार्गदर्शक लेख संकलित हैं। ये लेख अपने समय की राजनीति और भाषा के चरित्र का उत्खनन करते हैं और उनका सच सामने लाते हैं। इन लेखों में लालित्य निबन्धों जैसा लालित्य है। वे अश्लीलता और स्त्री जैसे संवेददशील विषय पर विचार करते हुए जिस निष्कर्ष पर पहुचते हैं, वह बहुत मानवीय है।
वे साहित्य और समाज पर बाजार के बढ़ते दवाबों को पूरी गम्भीरता से लेते हुए उसके अंजाम के प्रति सचेत करते हैं। कहना चाहें तो कह सकते हैं कि अपनी खास शैली में बे सोए हुए लोगों को जगाते हैं और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि प्रेमचंद उनके सर्वाधिक प्रिय लेखकों में हैं। यह अकारण नहीं है कि ‘उपन्यास का लोकतंत्र’ शीर्षक खण्ड में प्रेमचन्द पर केन्द्रित दो आलेख हैं और अन्य आलेखों में भी वे केन्द्रीय व्यक्तित्व की तरह उपस्थित हैं। इधर उपन्यास को लेकर जिन आलोचकों ने महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक कार्य किये हैं, मैनेजर पाण्डेय उनमें से एक हैं। उपन्यास और लोकतन्त्र जैसे प्राणवान लेख हाल के वर्षों में हिन्दी में नहीं लिखे गये हैं। यही बात ‘भारतीय उपन्यास की भारतीयता’ के संदर्भ में भी कही जा सकती है। यह महत्त्वपूर्ण है कि उपन्यासों पर लिखते हुए मैनेजर पाण्डेय प्रेमचन्द से लेकर रेणु, दूधनाथ सिंह, संजीव, मैत्रेयी पुष्पा, गीतांजलि श्री और कई अन्य नये उपन्यासकारों के उपन्यासों से गुजरते हैं।
पाण्डेय जी का लेखन कहीं से भी इकहरा नहीं है। वे अपनी बात को समझाने के लिए टालस्टॉय और टॉमस मान जैसे महान लेखकों को भी जिरह के बीच लाते हैं और इस प्रकार अपनी आलोचना को वृहत्तर अर्थवत्ता भी प्रदान करते हैं। वे इसी प्रकार जब समकालीन कविता पर बात करते हैं तो जनकवि नागार्जुन उन्हें चुनौती और आदर्श की तरह दिखाई देते हैं। वे युवा कवियों की पीठ आशीर्वाद की मुद्रा में नहीं थपथपाते बल्कि कुछ ठोस आधारों जैसे-साम्प्रदायिकता विरोध, सामाजिकता, शोषण और दमन की समझ, स्त्री और वंचित समाज के प्रति दृष्टिकोण और किसी हद तक कविता में कविता की रक्षा आदि पर उनका मूल्यांकन करते हुए कहीं प्रशंसा करते हैं तो कहीं ख़बर भी लेते हैं। आशंका और उम्मीद का द्वन्द्व बना रहता है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है तो यह कहना ज्यादा उचित होगा कि पाण्डेय जी की आलोचना भाषा में दार्शनिक गम्भीरता और सहजता का अद्भुत संयोग है। जहाँ वे सैद्धान्तिक बहस में शामिल होते हैं, वहाँ भाषा दार्शनिक स्वरूप ले लेती है और जहाँ वे व्यावहारिक आलोचना में रहते हैं, वहाँ भाषा किसी वेगवती पहाड़ी नदी का रूप ले लेती है। बिल्कुल सहज निर्मल। लेकिन इस सन्दर्भ में यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि वे जहाँ चाहते हैं, वहाँ भाषा रूपी नदी के वेग को अपने ढंग से मोड लेते हैं। यहाँ यह भी देखना सुखद है कि भाषा की परम्परा में वे रामचन्द्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह से जुड़ते हुए हिन्दी आलोचना की भाषा में उसमें बहुत कुछ नया जोड़ते हैं। वे रामचन्द्र शुक्ल के बाद सम्भवत: पहले आलोचक हैं, जिन्होंने कई आलोचनात्मक पदों (यथा-काव्यानुभूति की संस्कृति, कविता की कर्मभूमि आदि) का सृजन किया है। यह हिन्दी आलोचना को उनका बड़ा योगदान है। इस समय हिन्दी में मैनेजर पाण्डेय सम्भवतः अकेले ऐसे आलोचक हैं जिनकी आलोचना में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक आलोचना का मणिकांचन योग दिखाई देता है। उनकी आलोचना के विषय में यह कहना ज्यादा उचित होगा कि यह न तो आह-आह की आलोचना है और न वाह-वाह की। इस सम्यक आलोचना रूपी भवन में सन्तुलित वैचारिक दृष्टि की एक ऐसी खिड़की है जो मनुष्यधर्मी रचनात्मकता के भीतर आने में कोई रुकावट पैदा नहीं करती है। यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं कि मैनेजर पाण्डेय की यह आलोचना पुस्तक भी रचनाकारों, आलोचकों और विमर्श तथा मनुष्यता में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए आक्सीजन से कम नहीं है।
|
|||||


 i
i