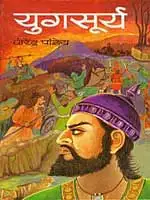|
ऐतिहासिक >> युगसूर्य युगसूर्यवीरेन्द्र पांडेय
|
19 पाठक हैं |
|||||||
राष्ट्र की अखंडता तथा भारत की संस्कृति पर केन्द्रित उपन्यास..
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रस्तुत उपन्यास के संबंध में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन ने
लेखक के नाम अपने एक मात्र पत्र में लिखा था, ‘जाहिर है कि इस
ऐतिहासिक उपन्यास को लिखने और तैयार करने में आपको अध्ययन व रिसर्च वगैरह
करने में काफी मेहनत करनी पड़ी होगी....इसे हिंदुस्तान के सभी हिंदू व
मुसलमानों को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि इसमें उन दोनों को उनके फर्जों की
याद दिलाई गई है..... बहुत से वाक्य ऐसे भी हैं, जिन्हें इनसान अपनी जाती
जिंदगी में उसूल के रूप में अख्तियार कर सकता है। एक अच्छी किताब लिखी हैं
आपने।’
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दिल्ली के तत्कालीन निदेशक डॉ. जीवन नायक ने इस कृति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए लेखक को लिखा था, ‘भारत में हिंदू- मुसलमानों की जटिल समस्याओं को समाधान की दिशा में सबसे पहली कोशिश बादशाह अकबर ने की थी, जो नाकामयाब रही। कालांतर में महात्मा गांधी ने भी; पर देश के बँटवारे को भी रोक न पाये। लेखक ने अपने उपन्यास में चिंतन की जो धारा दी है, मुझे वही मार्ग समझ मे आता है। मैं आपके इस उपन्यास को एक ऐसी अनूठी व सर्वोत्तम कृति के रूप में देखता हूँ, जिसका सर्वोपरि लक्ष्य राष्ट्र की अखंडता तथा भारत की संस्कृति को विश्न-भर में विशिष्टता प्रदान करना प्रतीत होता है।’
समर्पित है
यह उपन्यास
मेरे
हिंदुस्तानी मुसलमान भाईयों को
बाइज्जत और प्यार के साथ....
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दिल्ली के तत्कालीन निदेशक डॉ. जीवन नायक ने इस कृति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए लेखक को लिखा था, ‘भारत में हिंदू- मुसलमानों की जटिल समस्याओं को समाधान की दिशा में सबसे पहली कोशिश बादशाह अकबर ने की थी, जो नाकामयाब रही। कालांतर में महात्मा गांधी ने भी; पर देश के बँटवारे को भी रोक न पाये। लेखक ने अपने उपन्यास में चिंतन की जो धारा दी है, मुझे वही मार्ग समझ मे आता है। मैं आपके इस उपन्यास को एक ऐसी अनूठी व सर्वोत्तम कृति के रूप में देखता हूँ, जिसका सर्वोपरि लक्ष्य राष्ट्र की अखंडता तथा भारत की संस्कृति को विश्न-भर में विशिष्टता प्रदान करना प्रतीत होता है।’
समर्पित है
यह उपन्यास
मेरे
हिंदुस्तानी मुसलमान भाईयों को
बाइज्जत और प्यार के साथ....
प्राक्कथन
देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम मुझे विरासत में मिला है। इतिहास और
साहित्य के अध्ययन ने उसमें निरंतर वृद्धि की। 1942 के ‘भारत
छोड़ो
आंदोलन’ में हिस्सा लेने के फलस्वरूप मेरे नाम चार वारंट निकले।
साहसिकता का अभाव मुझसें कभी नहीं रहा। इसलिए, सिर झुकाकर जेलयात्रा करना
मेरे स्वभाव के विरुद्ध था। मैंने लगभग तीन वर्ष तक भूमिगत रहते हुए
फिरंगी पुलिस से आँख मिचौली खेलना ज्यादा पसंद किया। इन वर्षों में मुझे
अपने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में भ्रमण करने और भारतीय जनजीवन को निकट
से देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। लगभग सभी संप्रदायों और वर्णों के साथ
मैंने स्नेहमय जीवन बिताया और इसी दौर में मेरे मन मे दो बातें घर कर गईं।
एक तो यह कि संत रविदास पर तब तक कोई शोधग्रंथ नहीं लिखा गया था। सभी उस
महान संत के प्रति उदासीन थे। दूसरी बात यह थी कि देश के दो बड़े
समुदाय-हिंदू और मुसलमान- जब तक अपने-अपने पूर्वाग्रहों को त्यागकर
राष्ट्रीय महायज्ञ में जुटकर योगदान नहीं करेंगे, तब तक देश की एकता और
मजबूती एक दिवास्पप्न ही रहेगी।
पहला संकल्प मेरा सन् 1941 में पूरा हुआ, जब मैंने संत रविदास पर अपना शोधग्रंथ पूरा किया। ‘संत रविदास और उनका काव्य’ अपने विषय पर पहला शोधग्रंथ था और उसे प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत भी किया।
1947 में जब आजादी मिली, तब देश के बँटवारे का एक कड़वा घूँट हर किसी को पीना पड़ा था। आजादी के बाद सभी लोग, चाहे वे भारत के थे या पाकिस्तान के, अपने-अपने काम-धंधे में लगते गए। मैं भी लगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सर्वप्रथम साप्ताहिक मुखपत्र ‘हमारी बात’ का संपादन-कार्य मुझे इसलिए भी भाया, क्योंकि उसमें मुझे अध्ययन के लिए समय के साथ-साथ अभिव्यक्ति का माध्यम भी मिला। अधिकतर साथी सक्रिय राजनीति की ओर आकर्षित हुए; किंतु मुझे आजादी के साथ मिले कड़वे घूट की कड़वाहट सताती रही। यह प्रश्न मेरे मन में लगातार खटकता रहा कि देश के हिंदू और मुसलमान सच्चे अर्थों और भावनात्मक रूप में ‘हिंदुस्तानी’ क्यों नहीं बन पा रहे हैं। मैंने इतिहास का मंथन किया, दोनों धर्मों और उनके साहित्य का अध्ययन किया और आठवीं शताब्दी से लेकर बींसवी शताब्दी तक की राजनीति की गहराई के साथ समीक्षा की। अनेक तथ्य और कारण सामने आए, जिनपर मैंने बार-बार चिंतन-मनन किया।
उधर गृहस्थी का भार भी मेरे कंधों पर था। पेशा पत्रकारिता का था, जो उस जमाने में आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर हुआ करता था, जूझना पड़ा। राजनीति क्षेत्र के अनेक आकर्षण और सुअवसर सामने आए किंतु नैतिकता और ईमानदारी ने कभी उनकी ओर को स्वीकृति नहीं दी। सुख-सुविधा के लिए अपने निर्धारित पथ से हटता मेरे सिद्धांत के विरुद्ध था। आजादी और लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिए अनवरत लिखते और प्रचार करते रहने में ही मुझे देश के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति नजर आई। बीच में एक बार, जब मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मासिक पत्र ‘आर्थिक समीक्षा’ का संपादन कर रहा था, मुझे नई दिल्दी स्थिति अमेरिकी दूतावास की ‘सूचना-सेवा’ में हिंदी प्रकाशनों के संपादन का पद-भार सँभालने का प्रस्ताव मिला। गृहस्थी के भार और आर्थिक संकोच के कारण मेरा मन थोड़ा डगमगाया। हिम्मत बढ़ी तब जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहाँ जाने की अनुमति दे दी।
इस तरह मैंने अमेरिका सूचना-सेवा के हिंदी प्रकाशन विभाग में संपादन का पद सँभाला और लगभग तेरह-चौदह वर्ष बाद भारत के प्रति अमेरिका की नीति में परिवर्तन हुआ, तो मेरी राष्ट्रीय विचार धारा आड़े आई। मुझे उसको त्यागकर पुनः कलम का सिपाही बनना पड़ा। यह सच है कि दूतावास की सेवा के दौरान मुझे वेतन के रूप में एक खासी धनराशि मिलती थी और पद छोड़ते समय मेरे पास केवल अपनी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिर गाँधी का आश्वासन मात्र था। फिर भी मैंने यही महसूस किया कि मैं एक बड़े अनचाहे बोझ से मुक्त हो गया हूँ।
जैसी मुझे आशा थी, आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई और मुझे अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए फिर से कमर कसनी पड़ी। यही वह दौर था, जिसमें मुझे 1942 का अपना संकल्प याद आया। प्रस्तुत उपन्यास के तत्व पुनः मेरे दिल दिमाग में उभरने लगे। मुझे अपनी पुरानी धुन में लगते देर न लगी।
संक्षेप में, प्रस्तुत उपन्यास केवल उपन्यास लिखने के शौक का परिणाम नहीं है। वह एक लक्ष्य अथवा एक दृष्टि विशेष की देन है, जिसके द्वारा मैंने अपने राष्ट्र की सेवा करने की अपनी उत्कट लगन की पूर्ति का प्रयास किया है। वह क्या है, इसे उसको ध्यान से पढ़नेवाले ही भली प्रकार बता सकते हैं।
मैं अपने को महापंडित, प्रकांड विद्वान् अथवा आचार्य नहीं मानता; न मैं अपने को किसी शास्त्र विशेष का विशेषज्ञ मानता हूँ। मैं तो सीधे, सरल स्वभाववाला एक श्रमजीवी लेखक हूँ। आत्मप्रचार और साहित्यिक अखाड़ेबाजे से भी हमेशा दूर रहा हूँ चूँकी अपने देश और संस्कृति के प्रति मेरी निष्ठा है, इसलिए उस निष्ठा के प्रति अपने कर्तव्यपालन के रूप में मैं अपने पाठकों के सक्षम यह उपन्यास प्रस्तुत कर रहा हूँ।
उपन्यास का परिवेश और कथानक 1995 से 1203 ईस्वी के बीच का है। कुछ चरित्र ऐतिहासिक हैं, जैसे-सम्राट पृथ्वीराज मुहम्मद गोरी मीरहुसैनशाह, चित्रा और कवि चंदबरदाई आदि। कुछ काल्पनिक हैं, जैसे- मलिका अतीका, रघुवंश गुसाँई, माधव भट्ट आदि। मूल कथा अनेक काव्यों में अपने-अपने ढंग से वर्णित है। मैंने उसे अपने उपन्यास में अपने ढंग से प्रस्तुत किया है उसके अनेक तर्कसंगत कारण भी हैं। जहाँ तक धर्म- दर्शन और विचारों का संबंध है उन्हें मूल अथवा प्रामाणिक सूत्रों से ही लिया गया है। भाषा के मामले में यह बात ध्यान में रखी गई है कि संपर्क के उपरान्त कालांतर में ही उसमें तालमेल हो पाता है।
लेखक के नाते मैं इस उपन्यास के सभी पाठकों, समीक्षकों और मूल्यांकन कर्ताओं से सहानुभूति और संवेदना की अपेक्षा करता हूँ। यह एक राष्ट्रीय प्रयास है; देश के हित में बड़ी जटिल और विविध प्रकार की समस्याओं का सामाधान ढूँढ़ने का प्रयास। इसमें संभव है, कहीं कोई खामी रह गई हो उसके लिए क्षमा-याचना करने में मुझे विलंब होगा और न किसी प्रकार का संकोच।
एक बात और, प्रस्तुत उपन्यास की रचना बड़े ही गम्भीर संघर्षों व मानसिक तनाव के हितों में हुई है। पांडुलिपि बढ़ जाने के कारण अपने सहृदय एवं कृपालु प्रकाशन के आदेशानुसार इसमें लगभग दो सौ टाइप किए हुए पृष्ठ कम करने पड़े मैं सराहना करूँगा मैं इसके प्रकाशक श्री श्यामसुंदरजी के साहस की, जिन्होंने महँगाई के इस युग में मेरे जैसे श्रमजीवी लेखक के इतने बड़े उपन्यास को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रकाशित किया है, अन्यता मेरे जैसे स्वाभिमानी लेखक को आज कौन पूछता है ?
अपने पाठकों से यह अकिंचन लेखक कोई विशेष अपेक्षा न करके केवल इतनी आशा अवश्य करता है कि वे उपन्यास को पढ़ने के बाद उसके संबंध में मुझे अपनी सम्मति अवश्य भेंजे। मेरा पता नीचे दिया हुआ है। आशा है पाठकों का सहयोग मुझे अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।
पहला संकल्प मेरा सन् 1941 में पूरा हुआ, जब मैंने संत रविदास पर अपना शोधग्रंथ पूरा किया। ‘संत रविदास और उनका काव्य’ अपने विषय पर पहला शोधग्रंथ था और उसे प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत भी किया।
1947 में जब आजादी मिली, तब देश के बँटवारे का एक कड़वा घूँट हर किसी को पीना पड़ा था। आजादी के बाद सभी लोग, चाहे वे भारत के थे या पाकिस्तान के, अपने-अपने काम-धंधे में लगते गए। मैं भी लगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सर्वप्रथम साप्ताहिक मुखपत्र ‘हमारी बात’ का संपादन-कार्य मुझे इसलिए भी भाया, क्योंकि उसमें मुझे अध्ययन के लिए समय के साथ-साथ अभिव्यक्ति का माध्यम भी मिला। अधिकतर साथी सक्रिय राजनीति की ओर आकर्षित हुए; किंतु मुझे आजादी के साथ मिले कड़वे घूट की कड़वाहट सताती रही। यह प्रश्न मेरे मन में लगातार खटकता रहा कि देश के हिंदू और मुसलमान सच्चे अर्थों और भावनात्मक रूप में ‘हिंदुस्तानी’ क्यों नहीं बन पा रहे हैं। मैंने इतिहास का मंथन किया, दोनों धर्मों और उनके साहित्य का अध्ययन किया और आठवीं शताब्दी से लेकर बींसवी शताब्दी तक की राजनीति की गहराई के साथ समीक्षा की। अनेक तथ्य और कारण सामने आए, जिनपर मैंने बार-बार चिंतन-मनन किया।
उधर गृहस्थी का भार भी मेरे कंधों पर था। पेशा पत्रकारिता का था, जो उस जमाने में आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर हुआ करता था, जूझना पड़ा। राजनीति क्षेत्र के अनेक आकर्षण और सुअवसर सामने आए किंतु नैतिकता और ईमानदारी ने कभी उनकी ओर को स्वीकृति नहीं दी। सुख-सुविधा के लिए अपने निर्धारित पथ से हटता मेरे सिद्धांत के विरुद्ध था। आजादी और लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिए अनवरत लिखते और प्रचार करते रहने में ही मुझे देश के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति नजर आई। बीच में एक बार, जब मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मासिक पत्र ‘आर्थिक समीक्षा’ का संपादन कर रहा था, मुझे नई दिल्दी स्थिति अमेरिकी दूतावास की ‘सूचना-सेवा’ में हिंदी प्रकाशनों के संपादन का पद-भार सँभालने का प्रस्ताव मिला। गृहस्थी के भार और आर्थिक संकोच के कारण मेरा मन थोड़ा डगमगाया। हिम्मत बढ़ी तब जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहाँ जाने की अनुमति दे दी।
इस तरह मैंने अमेरिका सूचना-सेवा के हिंदी प्रकाशन विभाग में संपादन का पद सँभाला और लगभग तेरह-चौदह वर्ष बाद भारत के प्रति अमेरिका की नीति में परिवर्तन हुआ, तो मेरी राष्ट्रीय विचार धारा आड़े आई। मुझे उसको त्यागकर पुनः कलम का सिपाही बनना पड़ा। यह सच है कि दूतावास की सेवा के दौरान मुझे वेतन के रूप में एक खासी धनराशि मिलती थी और पद छोड़ते समय मेरे पास केवल अपनी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिर गाँधी का आश्वासन मात्र था। फिर भी मैंने यही महसूस किया कि मैं एक बड़े अनचाहे बोझ से मुक्त हो गया हूँ।
जैसी मुझे आशा थी, आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई और मुझे अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए फिर से कमर कसनी पड़ी। यही वह दौर था, जिसमें मुझे 1942 का अपना संकल्प याद आया। प्रस्तुत उपन्यास के तत्व पुनः मेरे दिल दिमाग में उभरने लगे। मुझे अपनी पुरानी धुन में लगते देर न लगी।
संक्षेप में, प्रस्तुत उपन्यास केवल उपन्यास लिखने के शौक का परिणाम नहीं है। वह एक लक्ष्य अथवा एक दृष्टि विशेष की देन है, जिसके द्वारा मैंने अपने राष्ट्र की सेवा करने की अपनी उत्कट लगन की पूर्ति का प्रयास किया है। वह क्या है, इसे उसको ध्यान से पढ़नेवाले ही भली प्रकार बता सकते हैं।
मैं अपने को महापंडित, प्रकांड विद्वान् अथवा आचार्य नहीं मानता; न मैं अपने को किसी शास्त्र विशेष का विशेषज्ञ मानता हूँ। मैं तो सीधे, सरल स्वभाववाला एक श्रमजीवी लेखक हूँ। आत्मप्रचार और साहित्यिक अखाड़ेबाजे से भी हमेशा दूर रहा हूँ चूँकी अपने देश और संस्कृति के प्रति मेरी निष्ठा है, इसलिए उस निष्ठा के प्रति अपने कर्तव्यपालन के रूप में मैं अपने पाठकों के सक्षम यह उपन्यास प्रस्तुत कर रहा हूँ।
उपन्यास का परिवेश और कथानक 1995 से 1203 ईस्वी के बीच का है। कुछ चरित्र ऐतिहासिक हैं, जैसे-सम्राट पृथ्वीराज मुहम्मद गोरी मीरहुसैनशाह, चित्रा और कवि चंदबरदाई आदि। कुछ काल्पनिक हैं, जैसे- मलिका अतीका, रघुवंश गुसाँई, माधव भट्ट आदि। मूल कथा अनेक काव्यों में अपने-अपने ढंग से वर्णित है। मैंने उसे अपने उपन्यास में अपने ढंग से प्रस्तुत किया है उसके अनेक तर्कसंगत कारण भी हैं। जहाँ तक धर्म- दर्शन और विचारों का संबंध है उन्हें मूल अथवा प्रामाणिक सूत्रों से ही लिया गया है। भाषा के मामले में यह बात ध्यान में रखी गई है कि संपर्क के उपरान्त कालांतर में ही उसमें तालमेल हो पाता है।
लेखक के नाते मैं इस उपन्यास के सभी पाठकों, समीक्षकों और मूल्यांकन कर्ताओं से सहानुभूति और संवेदना की अपेक्षा करता हूँ। यह एक राष्ट्रीय प्रयास है; देश के हित में बड़ी जटिल और विविध प्रकार की समस्याओं का सामाधान ढूँढ़ने का प्रयास। इसमें संभव है, कहीं कोई खामी रह गई हो उसके लिए क्षमा-याचना करने में मुझे विलंब होगा और न किसी प्रकार का संकोच।
एक बात और, प्रस्तुत उपन्यास की रचना बड़े ही गम्भीर संघर्षों व मानसिक तनाव के हितों में हुई है। पांडुलिपि बढ़ जाने के कारण अपने सहृदय एवं कृपालु प्रकाशन के आदेशानुसार इसमें लगभग दो सौ टाइप किए हुए पृष्ठ कम करने पड़े मैं सराहना करूँगा मैं इसके प्रकाशक श्री श्यामसुंदरजी के साहस की, जिन्होंने महँगाई के इस युग में मेरे जैसे श्रमजीवी लेखक के इतने बड़े उपन्यास को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रकाशित किया है, अन्यता मेरे जैसे स्वाभिमानी लेखक को आज कौन पूछता है ?
अपने पाठकों से यह अकिंचन लेखक कोई विशेष अपेक्षा न करके केवल इतनी आशा अवश्य करता है कि वे उपन्यास को पढ़ने के बाद उसके संबंध में मुझे अपनी सम्मति अवश्य भेंजे। मेरा पता नीचे दिया हुआ है। आशा है पाठकों का सहयोग मुझे अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।
वीरेंद्र पांडेय
एक
हिंदूकुश के गगनचुंबी शिखरों की ओट से चाँद झाँक रहा था। लालायित रश्मियाँ
भारत-भूमि पर बिखरने के लिए व्याकुल थीं यह स्वाभाविक अवरोधों ने राह
रोकने का प्रयत्न किया, किंतु धरती की उदारता ने स्वागत में हृदय बिछा
दिया। रश्मियाँ नाच उठीं। चाँद की चाँदनी भारतीय वसुंधरा पर प्रसार पाने
लगी।
‘चाँदनी’ का भी एक सौंदर्य था; किंतु ‘शस्यश्यामला’ के सौंदर्य में उसे विलीन होते देर न लगी। दोनों ने मिलकर एक ‘नए सौंदर्य’ की सृष्टि की-धरती चमक उठी और चाँदनी अपनी सार्थकता पर मुस्कुराने लगी।
जंगली झुरमुट की ओट, एक शिलाखंड पर लेटी चित्ररेखा ने करवट बदली। पश्चिमोत्तर की भूरी मटमैली पहाड़ियों को देखते-देखते भय और आशंकाओं से उसका अंग-अंग रोमांचित हो उठा। उसकी दृष्टि उन भयानक दैत्याकार गिरीश्रृंखलाओं पर अधिक देर तक न टिक सकी। उसने आँखे मीच लीं। और एक लंबे निश्श्वास के साथ उसके मुख से निकल पड़ा, ‘‘ओफ !’’
रात का द्वितीय प्रहर।
उत्थान-पतन के चिरंतन नियम की याद दिलाती हुई ऊँची-नीची चट्टानों और पथरीली असमतल भूमि।
कहीं घने वृक्षों के झुरमुट तो कहीं दूर-दूर तक वनस्पति का अभाव और शीत समीर के मंद स्वरों को भी स्पष्ट करनेवाली भयानक नीरवता।
चित्रा ने निस्सीम आकाश की ओर देखा। दोनों हाथों को सिर के नीचे रखकर वह चित लेट गई और ग्रह-नक्षत्रों की प्रतिपल घनी होती भीड़ को निरीह बालिका की भाँति निहारने लगी।
अकस्मात् एक तारा टूट गिरा दूर तक फिसलता-सा चला गया। ज्योति मंद पड़ती गई और देखते-देखते वह अस्तित्वहीन हो गया ।
चित्रा के अंतरतम की घनी भूत पीड़ा सजग हो उठी, होंठ बुदबुदा उठे- ‘‘यह भी कोई जीवन है !’’ स्मृतियाँ कुनकुना रही थीं। उसे याद आ रहा था-
वह भी तो पूर्णिमा की रात थी, जब सिंधु देश के समस्त बाल-वृद्ध पुरुष-स्त्री उसके दर्शनों के लिए राजप्रासाद के बाह्य प्रांगण में उमड़ आए थे। लगता था जैसे उनके सौंदर्य की एक झलक अथवा उसके कंठ का मात्र एक स्वर उनके जीवन को सौंदर्य एवं संगीत से आप्लावित करने के लिए पर्याप्त है।
सिंधु-नरेश भी उस दिन कितने प्रसन्न थे ! कला, काव्य और संगीत का वह अनन्य उपासक अपने देशवासियों के साथ उसकी कला को सम्मान देने के लिए कितना उत्सुक था !
राजनर्तकी की एकमात्र पुत्री उस दिन प्रथम बार सिंधु-नरेश और उनकी कलाप्रेमी जनता के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रही थी। उस दिन उसकी इक्कीसवीं वर्षगाँठ थी। सुधांशु की आभा जिस प्रकार उसके उदय होने के पहले ही फैल जाती है उसी देश उसी प्रकार चित्रा के सौंदर्य नृत्य तथा उसकी काव्याभिरुचि की प्रशस्ति सिंधु देश के कोने-कोने में ही नहीं अपितु उसकी सीमाओं के बाहर भी पहुँच चुकी थी।
‘चाँदनी’ का भी एक सौंदर्य था; किंतु ‘शस्यश्यामला’ के सौंदर्य में उसे विलीन होते देर न लगी। दोनों ने मिलकर एक ‘नए सौंदर्य’ की सृष्टि की-धरती चमक उठी और चाँदनी अपनी सार्थकता पर मुस्कुराने लगी।
जंगली झुरमुट की ओट, एक शिलाखंड पर लेटी चित्ररेखा ने करवट बदली। पश्चिमोत्तर की भूरी मटमैली पहाड़ियों को देखते-देखते भय और आशंकाओं से उसका अंग-अंग रोमांचित हो उठा। उसकी दृष्टि उन भयानक दैत्याकार गिरीश्रृंखलाओं पर अधिक देर तक न टिक सकी। उसने आँखे मीच लीं। और एक लंबे निश्श्वास के साथ उसके मुख से निकल पड़ा, ‘‘ओफ !’’
रात का द्वितीय प्रहर।
उत्थान-पतन के चिरंतन नियम की याद दिलाती हुई ऊँची-नीची चट्टानों और पथरीली असमतल भूमि।
कहीं घने वृक्षों के झुरमुट तो कहीं दूर-दूर तक वनस्पति का अभाव और शीत समीर के मंद स्वरों को भी स्पष्ट करनेवाली भयानक नीरवता।
चित्रा ने निस्सीम आकाश की ओर देखा। दोनों हाथों को सिर के नीचे रखकर वह चित लेट गई और ग्रह-नक्षत्रों की प्रतिपल घनी होती भीड़ को निरीह बालिका की भाँति निहारने लगी।
अकस्मात् एक तारा टूट गिरा दूर तक फिसलता-सा चला गया। ज्योति मंद पड़ती गई और देखते-देखते वह अस्तित्वहीन हो गया ।
चित्रा के अंतरतम की घनी भूत पीड़ा सजग हो उठी, होंठ बुदबुदा उठे- ‘‘यह भी कोई जीवन है !’’ स्मृतियाँ कुनकुना रही थीं। उसे याद आ रहा था-
वह भी तो पूर्णिमा की रात थी, जब सिंधु देश के समस्त बाल-वृद्ध पुरुष-स्त्री उसके दर्शनों के लिए राजप्रासाद के बाह्य प्रांगण में उमड़ आए थे। लगता था जैसे उनके सौंदर्य की एक झलक अथवा उसके कंठ का मात्र एक स्वर उनके जीवन को सौंदर्य एवं संगीत से आप्लावित करने के लिए पर्याप्त है।
सिंधु-नरेश भी उस दिन कितने प्रसन्न थे ! कला, काव्य और संगीत का वह अनन्य उपासक अपने देशवासियों के साथ उसकी कला को सम्मान देने के लिए कितना उत्सुक था !
राजनर्तकी की एकमात्र पुत्री उस दिन प्रथम बार सिंधु-नरेश और उनकी कलाप्रेमी जनता के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रही थी। उस दिन उसकी इक्कीसवीं वर्षगाँठ थी। सुधांशु की आभा जिस प्रकार उसके उदय होने के पहले ही फैल जाती है उसी देश उसी प्रकार चित्रा के सौंदर्य नृत्य तथा उसकी काव्याभिरुचि की प्रशस्ति सिंधु देश के कोने-कोने में ही नहीं अपितु उसकी सीमाओं के बाहर भी पहुँच चुकी थी।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i