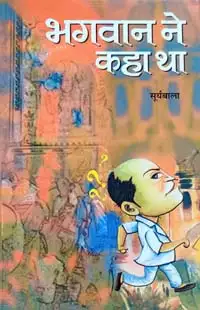|
कहानी संग्रह >> कात्यायनी संवाद कात्यायनी संवादसूर्यबाला
|
102 पाठक हैं |
|||||||
इन कहानियों में यथार्थ और सच्चाई को प्रस्तुत किया गया है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
ताता के मन में अँदेशा पैठ गया। दादी चली जाएगी। मम्मी-पापा भी तो कितनी
बार ऐसे ही कहते हैं, बाद में चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं।
दादी भी कीशनजी, राधाजी, घंटी, आरती सबकुछ लेकर चली जाएँगी। ताता के पास फिर से खूब भड़कीले रंगोंवाली ढेरमढेर किताबें, स्टफ-टॉयेज और तेज आवाज करने वाले भोपूँ बजाते हवाई जहाज, मोटर कारें, ट्रेन, चर्खियाँ रह जाएँगी और इस सबके बीच अकेली ताता...या फिर आया, बुड्डी अम्मा, बुड्डा बाबा...
अचानक वह वापस दादी के पास आई-
‘दादी ! तुम जाना मत। प्रॉमिश,’ दादी ने अचकचाकर देखा-ताता की आँखें दुबारा पूछ रही थीं-‘प्रॉमिश ? दादी-
ताता के अनजाने उसकी आँखें लबालब आँसुओं से भरी थीं।
इतने कीमती आँसू अरसे से किसी ने माँजी के लिए नहीं बहाए थे।
दादी भी कीशनजी, राधाजी, घंटी, आरती सबकुछ लेकर चली जाएँगी। ताता के पास फिर से खूब भड़कीले रंगोंवाली ढेरमढेर किताबें, स्टफ-टॉयेज और तेज आवाज करने वाले भोपूँ बजाते हवाई जहाज, मोटर कारें, ट्रेन, चर्खियाँ रह जाएँगी और इस सबके बीच अकेली ताता...या फिर आया, बुड्डी अम्मा, बुड्डा बाबा...
अचानक वह वापस दादी के पास आई-
‘दादी ! तुम जाना मत। प्रॉमिश,’ दादी ने अचकचाकर देखा-ताता की आँखें दुबारा पूछ रही थीं-‘प्रॉमिश ? दादी-
ताता के अनजाने उसकी आँखें लबालब आँसुओं से भरी थीं।
इतने कीमती आँसू अरसे से किसी ने माँजी के लिए नहीं बहाए थे।
इसी संग्रह से
सूर्यबाला की नवीनतम कहानियों का यह संकलन जीवन के यथार्थ और सचाई को
प्रस्तुत करता है और बहुत कुछ सोचने को विवश करता है।
लिखना क्यों ?...
कलम की नोक पर अड़ा एक हठी सवाल
उम्र और लेखन के इस पड़ाव तक आते-आते कितनी बार यह सवाल मेरा घेराव कर
चुका है। मुझे कटघरे में डाल चुका है। क्यों लिखती हूँ मैं
?—खुद की
खुद के साथ चलती एक अनवरत जिज्ञासा—भर नहीं—अड़ियल,
जिद्दी
बच्चे-सा हमेशा मेरे वजूद से अटकता, उलझता, अपने हठ पर अड़ा एक सवाल!
अचानक रुकती हूँ, उम्र की ढलान से उतरकर एक नन्ही-सी बच्ची में तब्दील हो जाती हूँ। दशकों लंबी तारकोली सड़क के किनारे चलती हुई, बस्ती के आखिरी छोर पर बने एक मकान के सामने वह बच्ची रुक जाती है।
उसके इस घर की पुख्ता मुँड़ेर की छोर पर भी पतंग-सा अटका है यह सवाल !
कटकर अटकी इस पतंग का छोर पकड़ूँ—कि माँझा सरक जाता है, हवा के साथ लहराती पतंग अदृश्य हो जाती है; ठीक इसी तरह, इस सवाल की डोर भी, जितना समेटने की कोशिश करती हूँ, हाथ से छूटती चली जाती है।
घरों की छतों और पेड़ों की फुनगियों पर उलझती, अटकती पतंग का पीछा करती वह बच्ची अचानक किन्हीं आवाजों का शोर सुनकर चौंक जाती है !
सामने, सड़क की दूसरी तरफ से बनारस के लिए जाती कोई अरथी गुजर रही होती है।
एक भयातुर सन्नाटा खिंच जाता है, बच्ची के मन-मस्तिष्क के आर-पार। दोपहरें तभी से निचाट, सन्नाटी लगती हैं, शामें उदास, खामोश। वह सन्नाटा आज तक मैं भर नहीं पाई हूँ। पाँचवीं-छठी में पढ़नेवाली दोनों बड़ी बहनें चीखती, शोर मचाती अपने-अपने बस्ते लिये स्कूल के लिए दौड़ जातीं। माँ नौकर-चाकरों के साथ घर का कामकाज, तोतली बहन और छुटके भाई को लेकर लस्त-पस्त हो जातीं। ऐसे में दोनों तरफ की जोड़-बाकी से बची हुई मैं, हर थोड़ी देर बाद अपनी ऊँचाई-बराबर की मुँड़ेर पर आकर खड़ी हो अचंभे और आतंक से भरी देखती रहती, हर घंटे, आधे घंटे पर इक्के पर, रिक्शे पर, कंधों पर और ‘अंतिम संस्कार मेल’ पर गुजरती अरथियाँ...
उनमें से कुछ गाजे-बाजे के साथ रेशमी परिधानों और रंग-बिरंगी झंडियों से सजी; खील, बतासे और ताँबे के पैसे लुटाती हुई; तो कुछ निपट अकेली इक्के या रिक्शों में बंधी, एकाध सहयात्री-भर साथ।
दोपहर में टिक्कड़-दाल खाकर अलसाते-ऊँघते नौकरों की आँखें अकसर इन विमानों की सजावट पर खुशी से टिहकार उठतीं।
प्रायः ऐसे ‘विमानों’ को किसी पेड़ के साए या चबूतरे पर उतारकर सहयात्री सुस्ताते होते। थोड़ी देर में ‘वैन’ आ जाती। काली वैन की छत के दोनों तरफ सफेद अक्षरों से लिखा होता ‘अंतिम संस्कार मेल’।
अरथी वैन की छत पर बाँध दी जाती। साथ जानेवाले बैठ जाते, बाकी भीड़ तितर-बितर हो जाती।
किसी ओर भी शोक-संतप्तता या अवसाद जैसा माहौल बिलकुल न होता—सिर्फ थकान, ऊब, एकरसता और समय काटने का-सा भाव। एक दहशत-भरा आतंक व्यापता जाता मेरी समूची बाल चेतना पर। मुँडे़रों के साये में घंटों चुपचाप बैठी, सहमी-सहमी-सी अपने आपसे पूछा करती—क्या होता है मरना—कैसे मर जाया जाता है ? क्या सचमुच एक दिन अम्मा, बाबूजी, बड़ी अम्मा, भैया और बहनें सब मर जाएँगे ?...इसी तरह ?...मैं भी ?...
नसों को जकड़ती हुई एक ठंडी सिहरन उतरती चली जाती।
मेरी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल हो गए इस सवाल और अहसास से घर के सारे बड़े लोग अनजान थे। उनकी नजरों में तो मैं एक बेहद चिबिल्ली और मजेदार शरारतों से भरपूर छोटी बच्ची थी।..
तो, ऊपर-ऊपर हाजिर-जवाब ठिठोलियों के कँगूरेदार बुर्ज और नीचे उफनता नहीं, गहराता चला जाता अवसादी समंदर—दो महाविरोधी वृत्तियों में जकड़ा हुआ बचपन। मेरे अंदर की खामोशी और आतंक सिर्फ मेरी चौदह वर्षीय बहन को छोड़कर और कोई न जान सका था। अब सोचती हूँ कि कितना परेशान कर दिया होगा मेरे आतंकित, डरे-सहमे प्रश्नों ने बारह-तेरह बरस की एक लड़की को; पर मेरी उस बड़ी बहन ने अपनी उम्र की सीमा से कहीं ज्यादा मुझे सँभाला और प्रबोधा था।
भय और आतंक छँटा...वह दहशत भी। जिन बहुत अपनों की मृत्यु की बात सोचकर ही एक रुँधती-सी सिहरन पसरती चली जाती थी। उनमें कितनों का चला जाना अब अतीत की एक घटना मात्र रह गई है। बीता समय पिटारी-सा बंद हो चुका है; पर सन्नाटा साथ लगा है। जैसे मैं उसी के बीच भटकती रहने के लिए जन्मी हूँ। जैसे मेरा वही सहमा हुआ पहला प्रश्न मुखौटा बदलकर मेरी कलम की नोक पर आकर टिक गया हो...
शुरुआती कुछ पंक्तियाँ ऐसी ही किसी मनःस्थिति में आप से आप बनती, रचती चली गई थीं। कोई वैराग्यशतक नहीं था वह। शायद उस अनाम बेकली को बाँट लेने की एक अवचेतती कोशिश-भर। किशोरवयी कहानियों और कविताओं में भी जाने-अनजाने, जहाँ-तहाँ झलकती चली गई अंदर बैठी यह खामोशी।
सचमुच सोचें तो लिखना है भी क्या ! एक सतत भटकन, एक अनवरत शोध...और इस दौरान मिल गए जवाबों को अलग-अलग खरादों पर जाँचते चले जाने की प्रक्रिया। पुनः प्रयोग और पुनः निदानों का एक अंतहीन सिलसिला।
जीवन भी तो कुछ इसी तरह है। एक अंतहीन यात्रा—पड़ाव बहुत सारे; पर दंतव्य कहीं नहीं। चलना, मात्र चलना। ठीक लिखने की तरह ही ! इस दृष्टि से लेखन और जीवन में बहुत कुछ सादृश्य-सा। दोनों एक- दूसरे से निरंतर पाते और बाँटते हुए गतिवान। महीन सुई की तरह यह कलम की नोक बेलबूटे काढ़ती चलती है, जिंदगी की चादर पर !...
यह कलम की नोक और कुछ नहीं, सिर्फ एक खरी नीयत और पक्के उसूल की माँग करती है। न जाने क्यों, आज हमने उसे आकाश छूती महत्त्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ दिया है। सृजन के मूल सुख, तृप्ति को दूसरा दरजा दे दिया है। उसे माध्यम बना लिया है, अपनी आकाशगामी, आकाशकामी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। साध्य से साधन हो गया यह लेख...वरना अपने आपको अक्षर-अक्षर रचते, बाँटते चलने की समूची प्रक्रिया ही कुछ इस तरह चलती है कि हम कहीं रह ही नहीं जाते। सब बाँट-बूँट बराबर। जीवन-स्वत्व का पूरी तरह शब्द के समत्व में समापन कर। रह जाता है तो बस अक्षर-शब्दों में समाया एक प्रार्थना रूप। मात्र अंजलि में रचा-बसा होता है—‘पाने’ और ‘बाँटने’ का अपूर्व समायोग।
एक बात और, हमें जो मिला, हम वही तो बाँटेंगे। मुझे दुःख और अवसाद मिला; लेकिन लाड़-दुलार से पोर-पोर सिंचा हुआ, अपनेपन में समोया हुआ। बेगाने के नाम से बिदकता हुआ...इस अवसाद को, दुःख को मैं नकारात्मक नहीं मान सकती। क्योंकि इसके माध्यम से मैं करुणा और अपनेपन की विरासत सहेजने और बाँटने की कोशिश करूँगी ही करूँगी। बीहड़ संकटों, संघर्षों में अपने टूटे रथ की धुरी पर कोहनी लगाने के लिए जो ममता-भरी बाँहें आगे आईं—जाने-अनजाने, वे सब भी उतरेंगे ही, लेखन के धर्मक्षेत्र में। और भी तो, हर मोड़, डगर पर कितने-कितने विलक्षण अहसास, भाव-संपदाएँ और अनजाने संबंधों के गहराते चले जाने वाले समंदर। इस समतल की अतल गहराई में जाने पर प्रायः लगता है, जीवन कितना अभेद तिलिस्म....भेदते चले जाइए, एक के बाद एक चोर दरवाजा खुलते चले जाएँगे। तिलिस्म गहराता चला जाएगा। और यह मन...मानव मन—(भगवान् बचाए इससे) हद का मोही, हद का निर्मम; पल में साधु, पल में महाप्रपंची चाटुकार...कभी सब कुछ लुटाकर बिछ जाने वाला तो कभी सबकुछ झपटकर हथिया लेने वाला—अनगिनत, असंख्य, खुले-अधखुले और जकड़ बंद प्रकोष्ठोंवाला, रेशमी परदे से ढँका एक नन्हा झरोखा—मैं प्रायः इस झरोखे से सटी देखती रह जाती हूँ—अर्जुन की तरह अपलक, अवाक्—इसमें निहित, अनंत विश्व ब्रह्मांड जैसी विस्मय-विमूढ़ कर देने वाली क्रिया-प्रक्रियाएँ, गतिविधियाँ। चुपचाप इन प्रकोष्ठों में घुसने की जासूसी मेरी कलम अनायास किया करती है।
यह इतना सच शायद अब तक हर रचना के उत्सबिंदु के रूप में चला आता है। जीवन का वह पहला अवसादी अहसास आज भी भरी पूरी महफिलों के बीच मुझमें पैठता चला जाता है। तो क्या निरंतर उस सन्नाटे को थहाते, खँगालते जाने के लिए लिखती हूँ ? प्रश्नवाचक चिह्न हटा लीजिए, उत्तर मिल जाएगा।
लेकिन यह कोई वजनदार, साहित्य की चौखट पर रखने लायक बात लगती नहीं। कुछ निरी वैयक्तिक और सीमित-सी। लेकिन यह न वैयक्तिक है, न सीमित ही। यह मन, यह उदासी एक नन्हा ताल है, जिसमें बहुत-बहुत सारे नामी-गिरामी चेहरों के अक्स हैं। जिनमें सिर्फ वे सब ही नहीं जो निरंतर संघर्ष करते हुए भी अपना प्राप्य नहीं प्राप्त कर पाए और जिंदगी, किन्ही अनाम वाजिब-गैरवाजिब कारणों से, उनकी छँटनी करती चली गई, बल्कि ‘वे’ भी जो इस जद्दोजहद में तार-तार होते जाने के बावजूद पूरे जीवट से अपनी उदासी छुपाए, अपनों के लिए ताउम्र मुसकराते चले गए। इस तरह के, दर्द को छुपाने में माहिर, लोगों ने मुझे भरी महफिलों में बहुत विकल किया है। उनकी हँसी मुझे इस हिचकोले खाती किश्ती की पतवार-सी लगी है जो अपने चारों ओर घिरी घुटन और दर्द की सतह को जी-जान से काटती चलती है।
मैं ऐसी ही मुसकराहटों की ओट से दुबक लेती हूँ—कलम की आड़ में—अपलक विस्मित देखती हूँ, गुमनाम तड़प के उस मुहरबंद इतिहास को जिसके सफे कभी न खुल पाने के लिए अभिशप्त हैं। दूसरे शब्दों में, इसे ही शायद अनकही पीड़ा का अभिषेक कहेंगे; हर रचनाकार से जीवन को मिलनेवाली करुणांजलि। आज से नहीं, आदि युग से—क्रौंचवध से पीड़ा से शुरू हुई ‘स्व’ को ‘लोक’ से मिलाती एक अजस्र धारा—व्यक्ति से व्यक्ति में, एक से अनेक में, प्रवहमान होती चली जाती है, हर किसी का अपना ही सच बनकर। लेखन की चरम उपलब्धि यही है। छोर-अछोर व्यक्ति-समाज से उसकी साझेदारी। यही उसका कार्य, यही उसका काम्य। ‘भुक्खड़ की औलाद’, ‘बाऊजी और ‘बंदर’, ‘न किन्नी न’, आदि ऐसे ही भावबिंदु से उपजी कहानियाँ हैं।
लेकिन यह साझेदारी पलायन और हताशा अँधेरे और अविश्वास की हो तो इसका औचित्य ? क्योंकि साहित्य को कभी समाज से निरपेक्ष देखा ही नहीं जा सकता। इसलिए सिर्फ खुदी की बुलंदी या खुदी के विलय पर विराम नहीं लगाया जा सकता। आपको हताशा, सन्नाटा और उदासी मिली है, तो मिली है; भुगतिए उसे—पर आप उसे वैसा का वैसा नहीं बाँट सकते। बाँटना है तो इस तरह कि उसी हताशा के बीच से जूझते हुए, दम से बेदम होते हुए भी बूँद-बूँद अमृत निचोड़ ले जाया जाए। हमारी चादर भले तार-तार हो गई हो, पर जिसका साझा है हमारे लेखन के साथ, उनमें अपनी उधड़ी सीवनें छुपाने नहीं, बल्कि गूँथ और सँवार ले जाने का हुनर थमा जाएँ। हदें उलाँघती भौतिकता, आज साहित्य को भले ही अप्रासंगिक मान बैठी हो प्रत्यक्ष जनजीवन के प्रवाह से, लेकिन साहित्य अपने सरोकारों के प्रति सन्नद्ध रहेगा ही रहेगा। प्रचार साधनों की क्रांति के इस नए युग में कलम से किसी क्रांति की उम्मीद तो एक दिवास्वप्न ही कही जाएगी। पर यह भी निश्चित है कि घोर विध्वंसगामी प्रवृत्तियों से निजात भी साहित्य ही दिला सकता है। क्रांति के रूप में न सही, क्रमशः व्यक्ति में से एक बेहतर व्यक्ति को ढालने की अनवरत कोशिश में। स्रोत भले ही हमारी करुणा, अवसाद और अँधेरा हो, समापन अविश्वास, अनास्था और अँधेरे के बीच नहीं वरन् जीवन-आस्था के आलोक बिंदु पर ही होना है। (‘गृहप्रवेश’ और ‘होगी जय...हे पुरुषोत्तम नवीन’)।
लेकिन इस अर्थ, इस लक्ष्य को मात्र कागजी अभियान, विद्रोह और जागृति तथा चेतना के शंखनाद के साथ जोड़ देने से पूरी बात अरचनात्मक—सी हो उठती है। इन शब्दों का बार-बार आलोड़न-विलोड़न और उछाल एक नकली आवेश को जन्म देकर रह जाता है। जबकि जरूरत आज एक मेच्योर समझ और बोध दे पाने की है।
पिछले दिनों ‘दीक्षांत’ (उपन्यास) लिखते हुए अंदर-अंदर कुछ ऐसी ही रस्साकशी चली। ‘दीक्षांत’ के नायक ‘शर्मा सर’ मर्मांतक, करुण परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और मैं उन्हें एक पॉजिटिव जीवन-दिशा नहीं दिखा पा रही। मैं उनके हाथों में विद्रोह की मशाल क्यों नहीं थमा पा रही ? क्यों नहीं क्रांति का बिगुल बजवा, न्याय की प्रतिष्ठा करा पा रही ? लेकिन नहीं करा पाई मैं ऐसा—क्योंकि शर्मा सर के आसपास की स्थितियाँ ऐसी नहीं थीं। अतः वह एक नकली, कागजी समाधान होता। साथ ही एक व्यक्ति/अध्यापक की करुण मृत्यु से उत्पन्न स्थितियों की निर्ममता भी उकेरनी थी। छात्रगुटों, यूनियन और निहित स्वार्थों के साथ वैयक्तिक स्तर पर व्याप्त संवेदनशून्यता और जड़ता भी उजागर करती थी...सब कुछ पूरा सच ही; किंतु इन सबके बावजूद व्यक्ति नाम से व्यक्ति के पूरे उठ गए विश्वास और संवेदनशून्यता को मन ने नहीं स्वीकारा। तब एक परिशिष्ट जोड़ा; जिसका उद्देश्य था—शर्मा सर के दोनों अनाथ बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का भार एक मेधावी छात्र के पिता द्वारा स्वेच्छा से ले लिया जाना। यह मात्र अपनी या अपने जैसे बहुत से पाठकों की राहत के लिए। फिर भी खतरा तो उठाया ही, ‘समर्थ चरित्र’ की स्थापना न करने का।
इस तरह नारी-जागरण, नारी-चेतना के इस युग में किसी मुखर, दबंग विद्रोही नारी-चरित्र की प्रतिष्ठा न करने का आरोप भी (‘मेरे संधिपत्र’, ‘यामिनी कथा) मुझपर लगता रहा है। मानती हूँ कि जीवन की स्थितियों को देखने से मेरी दृष्टि ज्यादा गांधीवादी रही है। मैं परिवर्तन और बेहतरी के लिए विद्रोह से पहले विवेक को रखती हूँ। विद्रोह की विध्वंसक भूमिका मुझे जीवनोपयोगी कभी नहीं लगी। अब भी मानती हूँ कि जीवन की बहुत कम स्थितियाँ ऐसी हैं जिन्हें विद्रोह के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। वहाँ अभी पाने से पहले देना होगा। विद्रोह से ऊपरी और कानूनी परिवर्तन ही ज्यादा किए जा सकते हैं, शायद किन्हीं हदों तक सुरक्षा और सुविधाएँ भी प्राप्त की जा सकती हैं; किन्तु जीवन के चरम-काम्य-सुख शांति और समरसता के संदर्भ में विद्रोह की भूमिका नगण्य ही होती है। व्यक्ति के मन-परिवर्तन दृष्टि-परिवर्तन के लिए कहीं अधिक संयम, संतुलन और धैर्य की आवश्यकता है। और आज यही जीवन से लुप्त होता जा रहा है।
नारी संदर्भों में तो अकसर यह बात विद्रूप में उड़ा दी जाती है कि युगों से सहते, संतुलन रखते क्या पाया हमने ?—लेकिन क्या उस ‘अति’ का उत्तर हम प्रतिस्पर्धा ‘अति’ से नहीं दे रहे ?—आवश्यकता इन ‘स्थितियों और व्यवस्थाओं के विरोध और विद्रोह की भूमिका से पूरी तरह सहमत होते हुए भी व्यक्ति के संवेदात्मक ह्रास की चिंता भी उतनी ही प्रासंगिक है। नारी-अस्मिता, नारी-मुक्ति और स्वातंत्र्य आज की सबसे बड़ी चुनौती है; लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि हम विश्व को बचा ले जाएँ। लेकिन प्रकृति और अपनी परंपरा से मिले कुछ दुर्लभ गुणों को गिरवी रखकर नहीं। अब तक यह अच्छी तरह समझ लेना है कि पुराना सब कुछ पिछड़ा ही नहीं। इसलिए ‘शुभ’, स्वस्थ संस्कारों को अंधे कुएँ में डालकर भी नहीं। त्याग-निष्ठा, संयम, धैर्य और विवेक एक युग विशेष के लिए उपयुक्त हों और दूसरे के लिए अनुपयुक्त, ऐसा नहीं है—वे हर युग के सत्य हैं और अगर आज इन्हें नकारा या अस्वीकारा जा रहा है, इन्हें झुठलाने की बचकानी कोशिशें की जा रही हैं तो उस सबसे विद्रोह भी हमारी रचनात्मकता का एक अंग होना चाहिए।
बह गई मैं। हँसेगे लोग कि फिर वही त्याग, आस्था, सब्र जैसे शब्दों की तोतारटंत ! लेकिन मात्र नारी के लिए नहीं, एक सम्पूर्ण व्यक्ति-संदर्भ में, आनेवाली पीढ़ी के लिए विशेषरूप से इन शब्दों की पुनः पड़ताल और परिभाषा आवश्यक है। क्योंकि सारी भौतिक उपलब्धियों के बाद भी जब व्यक्ति बेहद रीता और खाली महसूस करता है, (पश्चिम की अति-भौतिकता के परिणाम और नई पीढ़ी का भटकना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है) तब वह अघाया, ऊबा और थका मन इन्हीं शब्दों के आसपास कहीं लंगर डालना चाहता है। एक बात और, जैसा प्रायः समझ लिया जाता है, ये शब्द कहीं से भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्मिता और चेतना के मार्ग में अवरोधक नहीं वरन् सहायक हैं। हमें सही निर्णय की सामर्थ्य और आत्मविश्वास सौंपनेवाले हैं, यह सब कहने का अर्थ ‘आक्रोश’ और विद्रोह की भूमिका को नकारना भी बिलकुल नहीं है। प्रायः मैं स्वयं ऐसे चरित्रों, स्थितियों के सान्निध्य में आई हूँ जब लगा है ‘विद्रोह’ ही एकमात्र विकल्प है, इस घुटन से मुक्ति का। क्योंकि सारे अन्य हथियार निरस्त हो चुके हैं। लेकिन यह निर्णय अन्य सभी अस्त्रों के उपयोग के बाद ही लिया जाना ठीक लगता है।
लेखकीय प्रकृति और संस्कारों का भी बड़ा हस्तक्षेप होता है रचनाधर्म में। उसके बाद उम्र के पड़ाव-दर-पड़ाव मिलते अनुभवों के पाथेय का। जहाँ तक मेरा सवाल है, जैसाकि पहले ही कहा है, मानवीय संबंधों की बड़ी ऊष्मा-भरी विरासत मिली है मुझे। जिंदगी जैसे आस्था के फूलों की एक पिटारी-सी, मोहबंधों के रेशमी बूटों से गुँथी-गथी। विराग की कल्पना मुझे आतंकित करती है, संन्यास मुझे सबसे बड़ा छद्म या चरम लाचारी की करुण परिणति लगता है।
बस, जिंदगी की यह बहुत तल्ख, बहुत करुण, बहुत मीठी किताब, मैं डूब-डूबकर पढ़ती और उसकी प्रूफ रीडिंग करती हूँ। अपने हिसाब से गलत-सही भी महसूसी। कितनी चीजें सीधे-साधे ब्रैकेट में डाल दीं—कितनी जगह कॉमा, सेमीकोलन और डैश से काम चलाया—विराम तो किसी और के हाथ में।
3, नरेंद्र भवन,
51, भूलाभाई देसाई मार्ग
बंबई-26
अचानक रुकती हूँ, उम्र की ढलान से उतरकर एक नन्ही-सी बच्ची में तब्दील हो जाती हूँ। दशकों लंबी तारकोली सड़क के किनारे चलती हुई, बस्ती के आखिरी छोर पर बने एक मकान के सामने वह बच्ची रुक जाती है।
उसके इस घर की पुख्ता मुँड़ेर की छोर पर भी पतंग-सा अटका है यह सवाल !
कटकर अटकी इस पतंग का छोर पकड़ूँ—कि माँझा सरक जाता है, हवा के साथ लहराती पतंग अदृश्य हो जाती है; ठीक इसी तरह, इस सवाल की डोर भी, जितना समेटने की कोशिश करती हूँ, हाथ से छूटती चली जाती है।
घरों की छतों और पेड़ों की फुनगियों पर उलझती, अटकती पतंग का पीछा करती वह बच्ची अचानक किन्हीं आवाजों का शोर सुनकर चौंक जाती है !
सामने, सड़क की दूसरी तरफ से बनारस के लिए जाती कोई अरथी गुजर रही होती है।
एक भयातुर सन्नाटा खिंच जाता है, बच्ची के मन-मस्तिष्क के आर-पार। दोपहरें तभी से निचाट, सन्नाटी लगती हैं, शामें उदास, खामोश। वह सन्नाटा आज तक मैं भर नहीं पाई हूँ। पाँचवीं-छठी में पढ़नेवाली दोनों बड़ी बहनें चीखती, शोर मचाती अपने-अपने बस्ते लिये स्कूल के लिए दौड़ जातीं। माँ नौकर-चाकरों के साथ घर का कामकाज, तोतली बहन और छुटके भाई को लेकर लस्त-पस्त हो जातीं। ऐसे में दोनों तरफ की जोड़-बाकी से बची हुई मैं, हर थोड़ी देर बाद अपनी ऊँचाई-बराबर की मुँड़ेर पर आकर खड़ी हो अचंभे और आतंक से भरी देखती रहती, हर घंटे, आधे घंटे पर इक्के पर, रिक्शे पर, कंधों पर और ‘अंतिम संस्कार मेल’ पर गुजरती अरथियाँ...
उनमें से कुछ गाजे-बाजे के साथ रेशमी परिधानों और रंग-बिरंगी झंडियों से सजी; खील, बतासे और ताँबे के पैसे लुटाती हुई; तो कुछ निपट अकेली इक्के या रिक्शों में बंधी, एकाध सहयात्री-भर साथ।
दोपहर में टिक्कड़-दाल खाकर अलसाते-ऊँघते नौकरों की आँखें अकसर इन विमानों की सजावट पर खुशी से टिहकार उठतीं।
प्रायः ऐसे ‘विमानों’ को किसी पेड़ के साए या चबूतरे पर उतारकर सहयात्री सुस्ताते होते। थोड़ी देर में ‘वैन’ आ जाती। काली वैन की छत के दोनों तरफ सफेद अक्षरों से लिखा होता ‘अंतिम संस्कार मेल’।
अरथी वैन की छत पर बाँध दी जाती। साथ जानेवाले बैठ जाते, बाकी भीड़ तितर-बितर हो जाती।
किसी ओर भी शोक-संतप्तता या अवसाद जैसा माहौल बिलकुल न होता—सिर्फ थकान, ऊब, एकरसता और समय काटने का-सा भाव। एक दहशत-भरा आतंक व्यापता जाता मेरी समूची बाल चेतना पर। मुँडे़रों के साये में घंटों चुपचाप बैठी, सहमी-सहमी-सी अपने आपसे पूछा करती—क्या होता है मरना—कैसे मर जाया जाता है ? क्या सचमुच एक दिन अम्मा, बाबूजी, बड़ी अम्मा, भैया और बहनें सब मर जाएँगे ?...इसी तरह ?...मैं भी ?...
नसों को जकड़ती हुई एक ठंडी सिहरन उतरती चली जाती।
मेरी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल हो गए इस सवाल और अहसास से घर के सारे बड़े लोग अनजान थे। उनकी नजरों में तो मैं एक बेहद चिबिल्ली और मजेदार शरारतों से भरपूर छोटी बच्ची थी।..
तो, ऊपर-ऊपर हाजिर-जवाब ठिठोलियों के कँगूरेदार बुर्ज और नीचे उफनता नहीं, गहराता चला जाता अवसादी समंदर—दो महाविरोधी वृत्तियों में जकड़ा हुआ बचपन। मेरे अंदर की खामोशी और आतंक सिर्फ मेरी चौदह वर्षीय बहन को छोड़कर और कोई न जान सका था। अब सोचती हूँ कि कितना परेशान कर दिया होगा मेरे आतंकित, डरे-सहमे प्रश्नों ने बारह-तेरह बरस की एक लड़की को; पर मेरी उस बड़ी बहन ने अपनी उम्र की सीमा से कहीं ज्यादा मुझे सँभाला और प्रबोधा था।
भय और आतंक छँटा...वह दहशत भी। जिन बहुत अपनों की मृत्यु की बात सोचकर ही एक रुँधती-सी सिहरन पसरती चली जाती थी। उनमें कितनों का चला जाना अब अतीत की एक घटना मात्र रह गई है। बीता समय पिटारी-सा बंद हो चुका है; पर सन्नाटा साथ लगा है। जैसे मैं उसी के बीच भटकती रहने के लिए जन्मी हूँ। जैसे मेरा वही सहमा हुआ पहला प्रश्न मुखौटा बदलकर मेरी कलम की नोक पर आकर टिक गया हो...
शुरुआती कुछ पंक्तियाँ ऐसी ही किसी मनःस्थिति में आप से आप बनती, रचती चली गई थीं। कोई वैराग्यशतक नहीं था वह। शायद उस अनाम बेकली को बाँट लेने की एक अवचेतती कोशिश-भर। किशोरवयी कहानियों और कविताओं में भी जाने-अनजाने, जहाँ-तहाँ झलकती चली गई अंदर बैठी यह खामोशी।
सचमुच सोचें तो लिखना है भी क्या ! एक सतत भटकन, एक अनवरत शोध...और इस दौरान मिल गए जवाबों को अलग-अलग खरादों पर जाँचते चले जाने की प्रक्रिया। पुनः प्रयोग और पुनः निदानों का एक अंतहीन सिलसिला।
जीवन भी तो कुछ इसी तरह है। एक अंतहीन यात्रा—पड़ाव बहुत सारे; पर दंतव्य कहीं नहीं। चलना, मात्र चलना। ठीक लिखने की तरह ही ! इस दृष्टि से लेखन और जीवन में बहुत कुछ सादृश्य-सा। दोनों एक- दूसरे से निरंतर पाते और बाँटते हुए गतिवान। महीन सुई की तरह यह कलम की नोक बेलबूटे काढ़ती चलती है, जिंदगी की चादर पर !...
यह कलम की नोक और कुछ नहीं, सिर्फ एक खरी नीयत और पक्के उसूल की माँग करती है। न जाने क्यों, आज हमने उसे आकाश छूती महत्त्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ दिया है। सृजन के मूल सुख, तृप्ति को दूसरा दरजा दे दिया है। उसे माध्यम बना लिया है, अपनी आकाशगामी, आकाशकामी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। साध्य से साधन हो गया यह लेख...वरना अपने आपको अक्षर-अक्षर रचते, बाँटते चलने की समूची प्रक्रिया ही कुछ इस तरह चलती है कि हम कहीं रह ही नहीं जाते। सब बाँट-बूँट बराबर। जीवन-स्वत्व का पूरी तरह शब्द के समत्व में समापन कर। रह जाता है तो बस अक्षर-शब्दों में समाया एक प्रार्थना रूप। मात्र अंजलि में रचा-बसा होता है—‘पाने’ और ‘बाँटने’ का अपूर्व समायोग।
एक बात और, हमें जो मिला, हम वही तो बाँटेंगे। मुझे दुःख और अवसाद मिला; लेकिन लाड़-दुलार से पोर-पोर सिंचा हुआ, अपनेपन में समोया हुआ। बेगाने के नाम से बिदकता हुआ...इस अवसाद को, दुःख को मैं नकारात्मक नहीं मान सकती। क्योंकि इसके माध्यम से मैं करुणा और अपनेपन की विरासत सहेजने और बाँटने की कोशिश करूँगी ही करूँगी। बीहड़ संकटों, संघर्षों में अपने टूटे रथ की धुरी पर कोहनी लगाने के लिए जो ममता-भरी बाँहें आगे आईं—जाने-अनजाने, वे सब भी उतरेंगे ही, लेखन के धर्मक्षेत्र में। और भी तो, हर मोड़, डगर पर कितने-कितने विलक्षण अहसास, भाव-संपदाएँ और अनजाने संबंधों के गहराते चले जाने वाले समंदर। इस समतल की अतल गहराई में जाने पर प्रायः लगता है, जीवन कितना अभेद तिलिस्म....भेदते चले जाइए, एक के बाद एक चोर दरवाजा खुलते चले जाएँगे। तिलिस्म गहराता चला जाएगा। और यह मन...मानव मन—(भगवान् बचाए इससे) हद का मोही, हद का निर्मम; पल में साधु, पल में महाप्रपंची चाटुकार...कभी सब कुछ लुटाकर बिछ जाने वाला तो कभी सबकुछ झपटकर हथिया लेने वाला—अनगिनत, असंख्य, खुले-अधखुले और जकड़ बंद प्रकोष्ठोंवाला, रेशमी परदे से ढँका एक नन्हा झरोखा—मैं प्रायः इस झरोखे से सटी देखती रह जाती हूँ—अर्जुन की तरह अपलक, अवाक्—इसमें निहित, अनंत विश्व ब्रह्मांड जैसी विस्मय-विमूढ़ कर देने वाली क्रिया-प्रक्रियाएँ, गतिविधियाँ। चुपचाप इन प्रकोष्ठों में घुसने की जासूसी मेरी कलम अनायास किया करती है।
यह इतना सच शायद अब तक हर रचना के उत्सबिंदु के रूप में चला आता है। जीवन का वह पहला अवसादी अहसास आज भी भरी पूरी महफिलों के बीच मुझमें पैठता चला जाता है। तो क्या निरंतर उस सन्नाटे को थहाते, खँगालते जाने के लिए लिखती हूँ ? प्रश्नवाचक चिह्न हटा लीजिए, उत्तर मिल जाएगा।
लेकिन यह कोई वजनदार, साहित्य की चौखट पर रखने लायक बात लगती नहीं। कुछ निरी वैयक्तिक और सीमित-सी। लेकिन यह न वैयक्तिक है, न सीमित ही। यह मन, यह उदासी एक नन्हा ताल है, जिसमें बहुत-बहुत सारे नामी-गिरामी चेहरों के अक्स हैं। जिनमें सिर्फ वे सब ही नहीं जो निरंतर संघर्ष करते हुए भी अपना प्राप्य नहीं प्राप्त कर पाए और जिंदगी, किन्ही अनाम वाजिब-गैरवाजिब कारणों से, उनकी छँटनी करती चली गई, बल्कि ‘वे’ भी जो इस जद्दोजहद में तार-तार होते जाने के बावजूद पूरे जीवट से अपनी उदासी छुपाए, अपनों के लिए ताउम्र मुसकराते चले गए। इस तरह के, दर्द को छुपाने में माहिर, लोगों ने मुझे भरी महफिलों में बहुत विकल किया है। उनकी हँसी मुझे इस हिचकोले खाती किश्ती की पतवार-सी लगी है जो अपने चारों ओर घिरी घुटन और दर्द की सतह को जी-जान से काटती चलती है।
मैं ऐसी ही मुसकराहटों की ओट से दुबक लेती हूँ—कलम की आड़ में—अपलक विस्मित देखती हूँ, गुमनाम तड़प के उस मुहरबंद इतिहास को जिसके सफे कभी न खुल पाने के लिए अभिशप्त हैं। दूसरे शब्दों में, इसे ही शायद अनकही पीड़ा का अभिषेक कहेंगे; हर रचनाकार से जीवन को मिलनेवाली करुणांजलि। आज से नहीं, आदि युग से—क्रौंचवध से पीड़ा से शुरू हुई ‘स्व’ को ‘लोक’ से मिलाती एक अजस्र धारा—व्यक्ति से व्यक्ति में, एक से अनेक में, प्रवहमान होती चली जाती है, हर किसी का अपना ही सच बनकर। लेखन की चरम उपलब्धि यही है। छोर-अछोर व्यक्ति-समाज से उसकी साझेदारी। यही उसका कार्य, यही उसका काम्य। ‘भुक्खड़ की औलाद’, ‘बाऊजी और ‘बंदर’, ‘न किन्नी न’, आदि ऐसे ही भावबिंदु से उपजी कहानियाँ हैं।
लेकिन यह साझेदारी पलायन और हताशा अँधेरे और अविश्वास की हो तो इसका औचित्य ? क्योंकि साहित्य को कभी समाज से निरपेक्ष देखा ही नहीं जा सकता। इसलिए सिर्फ खुदी की बुलंदी या खुदी के विलय पर विराम नहीं लगाया जा सकता। आपको हताशा, सन्नाटा और उदासी मिली है, तो मिली है; भुगतिए उसे—पर आप उसे वैसा का वैसा नहीं बाँट सकते। बाँटना है तो इस तरह कि उसी हताशा के बीच से जूझते हुए, दम से बेदम होते हुए भी बूँद-बूँद अमृत निचोड़ ले जाया जाए। हमारी चादर भले तार-तार हो गई हो, पर जिसका साझा है हमारे लेखन के साथ, उनमें अपनी उधड़ी सीवनें छुपाने नहीं, बल्कि गूँथ और सँवार ले जाने का हुनर थमा जाएँ। हदें उलाँघती भौतिकता, आज साहित्य को भले ही अप्रासंगिक मान बैठी हो प्रत्यक्ष जनजीवन के प्रवाह से, लेकिन साहित्य अपने सरोकारों के प्रति सन्नद्ध रहेगा ही रहेगा। प्रचार साधनों की क्रांति के इस नए युग में कलम से किसी क्रांति की उम्मीद तो एक दिवास्वप्न ही कही जाएगी। पर यह भी निश्चित है कि घोर विध्वंसगामी प्रवृत्तियों से निजात भी साहित्य ही दिला सकता है। क्रांति के रूप में न सही, क्रमशः व्यक्ति में से एक बेहतर व्यक्ति को ढालने की अनवरत कोशिश में। स्रोत भले ही हमारी करुणा, अवसाद और अँधेरा हो, समापन अविश्वास, अनास्था और अँधेरे के बीच नहीं वरन् जीवन-आस्था के आलोक बिंदु पर ही होना है। (‘गृहप्रवेश’ और ‘होगी जय...हे पुरुषोत्तम नवीन’)।
लेकिन इस अर्थ, इस लक्ष्य को मात्र कागजी अभियान, विद्रोह और जागृति तथा चेतना के शंखनाद के साथ जोड़ देने से पूरी बात अरचनात्मक—सी हो उठती है। इन शब्दों का बार-बार आलोड़न-विलोड़न और उछाल एक नकली आवेश को जन्म देकर रह जाता है। जबकि जरूरत आज एक मेच्योर समझ और बोध दे पाने की है।
पिछले दिनों ‘दीक्षांत’ (उपन्यास) लिखते हुए अंदर-अंदर कुछ ऐसी ही रस्साकशी चली। ‘दीक्षांत’ के नायक ‘शर्मा सर’ मर्मांतक, करुण परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और मैं उन्हें एक पॉजिटिव जीवन-दिशा नहीं दिखा पा रही। मैं उनके हाथों में विद्रोह की मशाल क्यों नहीं थमा पा रही ? क्यों नहीं क्रांति का बिगुल बजवा, न्याय की प्रतिष्ठा करा पा रही ? लेकिन नहीं करा पाई मैं ऐसा—क्योंकि शर्मा सर के आसपास की स्थितियाँ ऐसी नहीं थीं। अतः वह एक नकली, कागजी समाधान होता। साथ ही एक व्यक्ति/अध्यापक की करुण मृत्यु से उत्पन्न स्थितियों की निर्ममता भी उकेरनी थी। छात्रगुटों, यूनियन और निहित स्वार्थों के साथ वैयक्तिक स्तर पर व्याप्त संवेदनशून्यता और जड़ता भी उजागर करती थी...सब कुछ पूरा सच ही; किंतु इन सबके बावजूद व्यक्ति नाम से व्यक्ति के पूरे उठ गए विश्वास और संवेदनशून्यता को मन ने नहीं स्वीकारा। तब एक परिशिष्ट जोड़ा; जिसका उद्देश्य था—शर्मा सर के दोनों अनाथ बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का भार एक मेधावी छात्र के पिता द्वारा स्वेच्छा से ले लिया जाना। यह मात्र अपनी या अपने जैसे बहुत से पाठकों की राहत के लिए। फिर भी खतरा तो उठाया ही, ‘समर्थ चरित्र’ की स्थापना न करने का।
इस तरह नारी-जागरण, नारी-चेतना के इस युग में किसी मुखर, दबंग विद्रोही नारी-चरित्र की प्रतिष्ठा न करने का आरोप भी (‘मेरे संधिपत्र’, ‘यामिनी कथा) मुझपर लगता रहा है। मानती हूँ कि जीवन की स्थितियों को देखने से मेरी दृष्टि ज्यादा गांधीवादी रही है। मैं परिवर्तन और बेहतरी के लिए विद्रोह से पहले विवेक को रखती हूँ। विद्रोह की विध्वंसक भूमिका मुझे जीवनोपयोगी कभी नहीं लगी। अब भी मानती हूँ कि जीवन की बहुत कम स्थितियाँ ऐसी हैं जिन्हें विद्रोह के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। वहाँ अभी पाने से पहले देना होगा। विद्रोह से ऊपरी और कानूनी परिवर्तन ही ज्यादा किए जा सकते हैं, शायद किन्हीं हदों तक सुरक्षा और सुविधाएँ भी प्राप्त की जा सकती हैं; किन्तु जीवन के चरम-काम्य-सुख शांति और समरसता के संदर्भ में विद्रोह की भूमिका नगण्य ही होती है। व्यक्ति के मन-परिवर्तन दृष्टि-परिवर्तन के लिए कहीं अधिक संयम, संतुलन और धैर्य की आवश्यकता है। और आज यही जीवन से लुप्त होता जा रहा है।
नारी संदर्भों में तो अकसर यह बात विद्रूप में उड़ा दी जाती है कि युगों से सहते, संतुलन रखते क्या पाया हमने ?—लेकिन क्या उस ‘अति’ का उत्तर हम प्रतिस्पर्धा ‘अति’ से नहीं दे रहे ?—आवश्यकता इन ‘स्थितियों और व्यवस्थाओं के विरोध और विद्रोह की भूमिका से पूरी तरह सहमत होते हुए भी व्यक्ति के संवेदात्मक ह्रास की चिंता भी उतनी ही प्रासंगिक है। नारी-अस्मिता, नारी-मुक्ति और स्वातंत्र्य आज की सबसे बड़ी चुनौती है; लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि हम विश्व को बचा ले जाएँ। लेकिन प्रकृति और अपनी परंपरा से मिले कुछ दुर्लभ गुणों को गिरवी रखकर नहीं। अब तक यह अच्छी तरह समझ लेना है कि पुराना सब कुछ पिछड़ा ही नहीं। इसलिए ‘शुभ’, स्वस्थ संस्कारों को अंधे कुएँ में डालकर भी नहीं। त्याग-निष्ठा, संयम, धैर्य और विवेक एक युग विशेष के लिए उपयुक्त हों और दूसरे के लिए अनुपयुक्त, ऐसा नहीं है—वे हर युग के सत्य हैं और अगर आज इन्हें नकारा या अस्वीकारा जा रहा है, इन्हें झुठलाने की बचकानी कोशिशें की जा रही हैं तो उस सबसे विद्रोह भी हमारी रचनात्मकता का एक अंग होना चाहिए।
बह गई मैं। हँसेगे लोग कि फिर वही त्याग, आस्था, सब्र जैसे शब्दों की तोतारटंत ! लेकिन मात्र नारी के लिए नहीं, एक सम्पूर्ण व्यक्ति-संदर्भ में, आनेवाली पीढ़ी के लिए विशेषरूप से इन शब्दों की पुनः पड़ताल और परिभाषा आवश्यक है। क्योंकि सारी भौतिक उपलब्धियों के बाद भी जब व्यक्ति बेहद रीता और खाली महसूस करता है, (पश्चिम की अति-भौतिकता के परिणाम और नई पीढ़ी का भटकना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है) तब वह अघाया, ऊबा और थका मन इन्हीं शब्दों के आसपास कहीं लंगर डालना चाहता है। एक बात और, जैसा प्रायः समझ लिया जाता है, ये शब्द कहीं से भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्मिता और चेतना के मार्ग में अवरोधक नहीं वरन् सहायक हैं। हमें सही निर्णय की सामर्थ्य और आत्मविश्वास सौंपनेवाले हैं, यह सब कहने का अर्थ ‘आक्रोश’ और विद्रोह की भूमिका को नकारना भी बिलकुल नहीं है। प्रायः मैं स्वयं ऐसे चरित्रों, स्थितियों के सान्निध्य में आई हूँ जब लगा है ‘विद्रोह’ ही एकमात्र विकल्प है, इस घुटन से मुक्ति का। क्योंकि सारे अन्य हथियार निरस्त हो चुके हैं। लेकिन यह निर्णय अन्य सभी अस्त्रों के उपयोग के बाद ही लिया जाना ठीक लगता है।
लेखकीय प्रकृति और संस्कारों का भी बड़ा हस्तक्षेप होता है रचनाधर्म में। उसके बाद उम्र के पड़ाव-दर-पड़ाव मिलते अनुभवों के पाथेय का। जहाँ तक मेरा सवाल है, जैसाकि पहले ही कहा है, मानवीय संबंधों की बड़ी ऊष्मा-भरी विरासत मिली है मुझे। जिंदगी जैसे आस्था के फूलों की एक पिटारी-सी, मोहबंधों के रेशमी बूटों से गुँथी-गथी। विराग की कल्पना मुझे आतंकित करती है, संन्यास मुझे सबसे बड़ा छद्म या चरम लाचारी की करुण परिणति लगता है।
बस, जिंदगी की यह बहुत तल्ख, बहुत करुण, बहुत मीठी किताब, मैं डूब-डूबकर पढ़ती और उसकी प्रूफ रीडिंग करती हूँ। अपने हिसाब से गलत-सही भी महसूसी। कितनी चीजें सीधे-साधे ब्रैकेट में डाल दीं—कितनी जगह कॉमा, सेमीकोलन और डैश से काम चलाया—विराम तो किसी और के हाथ में।
3, नरेंद्र भवन,
51, भूलाभाई देसाई मार्ग
बंबई-26
-सूर्यबाला
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i