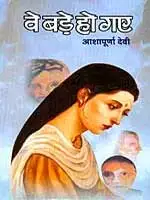|
नारी विमर्श >> वे बड़े हो गए वे बड़े हो गएआशापूर्णा देवी
|
369 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है उत्कृष्ठ उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रसिद्ध बँगला साहित्य उपन्यासकार श्रीमती आशापूर्णा देवी के इस उपन्यास
की मुख्य पात्र है सुलेखा, जो एक मध्य वर्गीय परिवार में पली-बढ़ी। बचपन
से ही पिता को खोने से उसे तथा उसकी बीमार माँ को चाचा की गृहस्थी में
शामिल होना पड़ा। बौद्धिक स्तर पर उन्नत होते हुए भी उसका मानसिक विकास न
हो सका। उसके चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ा उसकी माँ का, जो अपनी आर्थिक
दैहिक असमर्थता के कारण एक अपराध-बोध से ग्रस्त थी।
बचपन से ही सुलेखा को अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर दूसरों को सुखी रखने की साधना में लगना पड़ा। ऐसी स्थिति निरंतर बनी रही। विवाह के पश्चात् भी कोई फेर-बदल नहीं हुआ। फलत: उसका व्यक्तित्व हीन-भाव से दब गया; परन्तु यह हीन-भाव उसकी कोमल प्रवृत्तियों को सुखा न सका। वह ममता का सागर बनकर अपने परिवार की हर खुशी के लिए अपने निजी सुख-स्वार्थ की आहुति देती रही। उसकी यह निस्वार्थ सेवा भी बहुलांश में समालोचना से घिरी रही। उसके जीवन भर की यही आकांक्षा और अभिलाषा रही कि उसके बच्चे जब बड़े हो जायँगे तब वह मुक्त होकर स्वच्छंद गति से अपना जीवन जी पाएगी।
बचपन से ही सुलेखा को अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर दूसरों को सुखी रखने की साधना में लगना पड़ा। ऐसी स्थिति निरंतर बनी रही। विवाह के पश्चात् भी कोई फेर-बदल नहीं हुआ। फलत: उसका व्यक्तित्व हीन-भाव से दब गया; परन्तु यह हीन-भाव उसकी कोमल प्रवृत्तियों को सुखा न सका। वह ममता का सागर बनकर अपने परिवार की हर खुशी के लिए अपने निजी सुख-स्वार्थ की आहुति देती रही। उसकी यह निस्वार्थ सेवा भी बहुलांश में समालोचना से घिरी रही। उसके जीवन भर की यही आकांक्षा और अभिलाषा रही कि उसके बच्चे जब बड़े हो जायँगे तब वह मुक्त होकर स्वच्छंद गति से अपना जीवन जी पाएगी।
भूमिका
इस उपन्यास की मुख्य पात्र है सुलेखा, जो एक मध्यवर्गीय परिवार में पली,
बड़ी हुई। बचपन में ही पिता को खोकर उसे तथा उसकी बीमार माँ को चाचा की
गृहस्थी में शामिल होना पड़ा। बौद्धिक स्तर पर उन्नत होते हुए भी उसका
मानसिक विकास न हो सका। उसके चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ा उसकी माँ का, जो
अपनी आर्थिक दैहिक असमर्थता के कारण एक अपराध-बोध से ग्रस्त थी। बचपन से
ही उसे अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर दूसरों को सुखी रखने की साधना में लगना
पड़ा। ऐसी स्थिति निरंतर बनी रही। विवाह के उपरांत भी कोई फेर-बदल नहीं
हुआ। फलत: उसका व्यक्तित्व ही भाव से दब गया; परन्तु यह हीन-भावना उसकी
कोमल प्रवृत्तियों को सुखा न सका। वह ममता का सागर बनकर अपने परिवार की हर
खुशी के लिए अपने निजी-स्वार्थ की आहुति देती रही। उसकी यह निस्सवार्थ
सेवा में बहुलांश में समालोचन से घिरी रही। उसके जीवन भर कब यही साधना रही
कि उसके बच्चे बड़े हो जाएँगे तब वह मुक्त होकर स्वच्छंद गति से अपना जीवन
जी पाएगी।
मगर इस लक्ष्य की ओर बढ़ते-बढ़ते वह इतनी यांत्रिक हो गई कि जीवन से रस ग्रहण करना भूल गई। एक दिन जब लक्ष्य सामने आ गया तब उसे एहसास हुआ कि समाप्ति तक पहुँचाना ही सही ढंग से जीना नहीं है, जीवन की मिठास तो उसे हर पल जीने में है।
मगर इस लक्ष्य की ओर बढ़ते-बढ़ते वह इतनी यांत्रिक हो गई कि जीवन से रस ग्रहण करना भूल गई। एक दिन जब लक्ष्य सामने आ गया तब उसे एहसास हुआ कि समाप्ति तक पहुँचाना ही सही ढंग से जीना नहीं है, जीवन की मिठास तो उसे हर पल जीने में है।
वे बड़े हो गए
घर्र-घर्र, घर्र-घर्र।
चक्का ऐसे घूम रहा है जैसे हाथ से नहीं, बिजली से घूम रहा हो। हाथ में बिजली जैसी शक्ति भरकर चक्का चलाने से सुलेखा का कंधा दुख रहा था, फिर भी घुमाए चली जा रही थी चक्के को। और करती भी क्या ? कल शाम को ही इन सिले हुए कपड़ों की डिलिवरी जो देनी है। सुबह के समय तो घर के इतने काम रहते हैं कि साँस लेने तक की फुरसत नहीं मिलती। तो फिर किस बूते पर वह काम अधूरा छोड़कर उठ जाए ?
जिस तरह से भी हो, अभी खत्म कर डालना है। हालाँकि मन चंचल होता जा रहा है। घड़ी का काँटा भी मानो उछल-उछलकर आगे भाग रहा है। थोड़ी देर में दस बजेंगे। बस, सिलाई जिस हालत में भी हो, छोड़कर जाना पड़ेगा। रात के भोजन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी।
निशीथ नियमपरस्त है। उसके खाने के समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही दस बजे, यारों की महफिल उठाकर नीचे से ऊपर चला आता है। रात का खाना ऊपर के बरामदे में ही होता है। बच्चे रात में नीचे उतरना नहीं चाहते हैं। उतरने के आलस से कह देते हैं-भूख नहीं है।
देख-सुनकर यही इंतजाम कर लिया है सुलेखा ने। शाम से पहले ही सारा भोजन पकाकर ऊपर ले आती है और चाय-नाश्ता बनाने वाले स्टोव पर गरम-गरम रोटी सेंक लेती है।
इस इंतजाम के बाद देखा गया है कि सबको भूख लग रही है। मन-ही-मन हँसती है सुलेखा, मगर कह नहीं सकती। हँसी-हँसी में भी कह दे तो अभिमानी मझली बेटी अगले दिन ही बहाना बना देगी-नहीं खाना है, भूख नहीं है।
जब बच्चे छोटे थे, तब सुलेखा दिन-रात सोचा करती थी-उफ, किसी तरह ये बड़े हो जाएँ तो चैन की साँस लूँ।...ऐसा सोचती थी, क्योंकि अकेले जिम्मेदारी पर पाँच-पाँच बच्चों का झमेला कम तो नहीं ! दिन-रात के लिए नौकर-दाई रखने की हैसियत भी नहीं रही कभी।
कोई आधुनिक महिला शायद सुलेखा के बच्चों की संख्या सुनकर हैरान हो जाएगी, मगर सुलेखा के जमाने में ‘सुखी परिवार’ बनाने का सत्परामर्श बाजार में इतना चालू नहीं था।
इस प्रकार से बचपन में ही शादी हो गई थी। अर्थात् आजकल के हिसाब से नहीं तो उस जमाने में अठारह साल में कदम रखने वाली लड़की को दुल्हन बनाने के लिए छोटी नहीं समझी जाता था।
नहीं समझा जाता था, तभी तो ब्याह होते ही गृहस्थी की चक्की में लगा दिया गया था उसे। तब से वह उसे ही घुमाए चली जा रही है। इधर सचमुच अल्हड़ होने के कारण ही ज्ञान-वृद्धि होने से पहले ही कुल पाँच अबोध बच्चों की माँ बन बैठी है। पढ़ना-लिखना भी हुआ कहाँ। गरीब विधवा की संतान, चाचा के घर पली-बढ़ी। अपने दो-दो भतीजों को पढ़ाने-लिखाने में ही चाचा की नाक में दम तो भतीजी को पढ़ाने का सवाल ही कहाँ !
फीस के पैसे जमा नहीं हो सके मैट्रिक की पूरी परीक्षा भी न दे सकी सुलेखा। उसके बाद तो ईश्वर की अपार अनुकंपा से ब्याह हो गया। शक्ल-सूरत अच्छी थी, इसलिए कृपा करना भी आसान हो गया। अत¬¬ शिक्षा का प्रसार स्कूल की चारदीवारी तक ही रह गया।
मगर निशीथ रंजन तो पड़ा-लिखा युवक था। खैर, उसकी बात जाने दें। अब तो सुलेखा एड़ी-चोटी एक कर गृहस्थी की टूटी नाव को खींच-खींचकर किनारे के करीब आ ही चुकी है। अब अगर इंतजार है तो इस बात का कि नाव पर सवार लोग छलाँग भरकर किनारे उतर पड़ें और अपने-अपने रास्ते निकल जाएँ। अब आकर बीते हुए अनेक वर्षों की मूर्खता का हिसाब लगाना भी निरर्थक ही होगा।
और भी निरर्थक होगा-कौन अधिक मूर्ख था-इस बात पर तर्क उठाना ।
अब तो सबकुछ सुंदर है, सजा-सँवरा है। अब अगर बच्चों के बारे में कोई पूछताछ करे तो आराम से कहा जा सकता है-दो बेटे, तीन बेटियाँ हैं-बड़ा बेटा मेड़िकल स्टुडेंट है, अगले वर्ष फाइनल परीक्षा देगा। बड़ी बेटी ने बी.ए. पासकर बी.टी. पढ़ना आरंभ किया है। मझली बेटी बी.एस.सी. में पढ़ रही है, छोटी ने इस बार हायर सेंकेडरी की परीक्षा दी है और सबसे छोटा बेटा दसवीं कक्षा में है।
सुलझा हुआ परिवार है, जैसे मोहरे बिछाए हुए शतरंज की बिसात हो। बस, खेल शुरू करने भर की देर है।
मगर हैरत की बात तो यह है कि अब अक्सर सुलेखा को लगता है कि खेलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं लगता है कि ये पाँचों बच्चे जब छोटे थे, तभी जीवन और सरल था।
तब झंझट होता भी था तो उन्हें नहलाने-खिलानें में, उनके कपड़े और गुदड़ी बदलने में, उनकी जिद पूरी करने में हरदम निगरानी करने में। कोई खाट से गिर न जाए, कोई सड़क पर निकल न जाए। और क्या था ? और तो कुछ याद नहीं आता। फिर पता नहीं क्यों, सुलेखा दिन-रात सोचा करती थी।–उफ, ये किसी तरह बड़े हो जाएँ तो मैं चैन की साँस ले सकूँ।
क्या पाँचों की पाँच किस्म की जरूरतें होती थीं, इसीलिए ?
तब तो दो बच्चे दोपहर में स्कूल जाने लगे थे, बाकी तीनों सवेरे। उन्हें दस बजे के भीतर ही नहला-खिलाकर भेजना पड़ता था, इन दोनों को भी उसी समय तैयार कर देती थी। पहले इन्हें देखे या फिर उनके लिए चावल पकाने बैठे, समझ नहीं पाती थी वह। घर के प्रधान सदस्य को तो ठीक नौ बजे खाना तैयार चाहिए।
तब सुलेखा को लगता था कि पानी में कूदें या आग में ? कभी तो सोचती थी-उफ, ये बड़े-बड़े हो जाएँ किसी तरह।....सुबह के काम से निपटते ही सुबह के स्कूल से बच्चे वापस आ जाते थे। तब उन्हें पकड़कर नहला-खिलाकर सुलाना-मल्ल-युद्ध से कम था क्या ? अकसर सुलाने की वह कोशिश भी बेकार जाती थी। सुलेखा न सो पाती थी, न कुछ काम कर पाती थी। कहानी की किताब पढ़ना ? वह तो सपना था।
मगर किताब पढ़ने की कितनी चाहत थी उसमें। वैसे, उसी में जीवन का सही अर्थ मिल जाता था।
इसके लिए उसकी चेष्टाओं का अंत नहीं था, अंत नहीं था डाँट खाने का भी। फिर भी नशा छूटता नहीं था।
हाथ में कहानी की किताब देखते ही चाची बोल उठती थीं, ‘यह किताब फिर कहाँ से आ गई ?’
चाची बेजार होकर कहती थीं, ‘घर में एक लाइब्रेरी से तो किताबें आती ही रही हैं। फिर भी इसके घर, उसके घर जाकर किताब माँगकर लाना। पता नहीं ऐसा भी क्या नशा है ! क्यों ? मुझे भी तो कहानी-उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्या मैं मुहल्ले में घूम-घूमकर माँगती फिरती हूँ ? किताब लाइब्रेरी से मँगाकर पढ़ी जाती है, यही तो जानती हूँ।’
चाची तो केवल इतना जानती हैं, यह सुलेखा को अच्छी तरह मालूम है और यह भी जानती है कि चाची की धारणा से पसंद की चीज का आनंद धीरे-धीरे लेना चाहिए।
अत: लाइब्रेरी से किताब बदलकर ले आना महीने में कुल तीन-चार बार ही होता होगा। अगर किताब मोटी हुई तो और भी कम।
तो फिर ? सुलेखा के मन की भूख मिटाने के लिए महीने में सिर्फ दो-तीन पुस्तकें ? घर-घर से मँगवाकर लाए बिना चारा ही क्या ?
पाँच दिन भोजन किए बिना पड़ी रह सकती है सुलेखा आराम से, परन्तु पाँच दिन किताब के बिना ? वैसा जीवन तो मरुभूमि-सा ही कठिन और नीरस होगा।
अत: निरुपाय सुलेखा प्यास बुझाने की आस लेकर पड़ोस के घर जाकर पूछती है, ‘नीला चाची, आपने लाइब्रेरी से किताब बदली क्या ?’.....किसी और के घर जाकर कहती, ‘मौसीजी, फिर आ गई आपको परेशान करने। उस दिन विभूति बंदोपाध्याय की जो किताब पढ़ रही थी, पूरा पढ़ लिया क्या ?’......नहीं तो कभी मोड़ पर जाकर सामने वाले घर में सावधानी से पूछती है, ‘समीर चाचा घर पर हैं ?’
चक्का ऐसे घूम रहा है जैसे हाथ से नहीं, बिजली से घूम रहा हो। हाथ में बिजली जैसी शक्ति भरकर चक्का चलाने से सुलेखा का कंधा दुख रहा था, फिर भी घुमाए चली जा रही थी चक्के को। और करती भी क्या ? कल शाम को ही इन सिले हुए कपड़ों की डिलिवरी जो देनी है। सुबह के समय तो घर के इतने काम रहते हैं कि साँस लेने तक की फुरसत नहीं मिलती। तो फिर किस बूते पर वह काम अधूरा छोड़कर उठ जाए ?
जिस तरह से भी हो, अभी खत्म कर डालना है। हालाँकि मन चंचल होता जा रहा है। घड़ी का काँटा भी मानो उछल-उछलकर आगे भाग रहा है। थोड़ी देर में दस बजेंगे। बस, सिलाई जिस हालत में भी हो, छोड़कर जाना पड़ेगा। रात के भोजन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी।
निशीथ नियमपरस्त है। उसके खाने के समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही दस बजे, यारों की महफिल उठाकर नीचे से ऊपर चला आता है। रात का खाना ऊपर के बरामदे में ही होता है। बच्चे रात में नीचे उतरना नहीं चाहते हैं। उतरने के आलस से कह देते हैं-भूख नहीं है।
देख-सुनकर यही इंतजाम कर लिया है सुलेखा ने। शाम से पहले ही सारा भोजन पकाकर ऊपर ले आती है और चाय-नाश्ता बनाने वाले स्टोव पर गरम-गरम रोटी सेंक लेती है।
इस इंतजाम के बाद देखा गया है कि सबको भूख लग रही है। मन-ही-मन हँसती है सुलेखा, मगर कह नहीं सकती। हँसी-हँसी में भी कह दे तो अभिमानी मझली बेटी अगले दिन ही बहाना बना देगी-नहीं खाना है, भूख नहीं है।
जब बच्चे छोटे थे, तब सुलेखा दिन-रात सोचा करती थी-उफ, किसी तरह ये बड़े हो जाएँ तो चैन की साँस लूँ।...ऐसा सोचती थी, क्योंकि अकेले जिम्मेदारी पर पाँच-पाँच बच्चों का झमेला कम तो नहीं ! दिन-रात के लिए नौकर-दाई रखने की हैसियत भी नहीं रही कभी।
कोई आधुनिक महिला शायद सुलेखा के बच्चों की संख्या सुनकर हैरान हो जाएगी, मगर सुलेखा के जमाने में ‘सुखी परिवार’ बनाने का सत्परामर्श बाजार में इतना चालू नहीं था।
इस प्रकार से बचपन में ही शादी हो गई थी। अर्थात् आजकल के हिसाब से नहीं तो उस जमाने में अठारह साल में कदम रखने वाली लड़की को दुल्हन बनाने के लिए छोटी नहीं समझी जाता था।
नहीं समझा जाता था, तभी तो ब्याह होते ही गृहस्थी की चक्की में लगा दिया गया था उसे। तब से वह उसे ही घुमाए चली जा रही है। इधर सचमुच अल्हड़ होने के कारण ही ज्ञान-वृद्धि होने से पहले ही कुल पाँच अबोध बच्चों की माँ बन बैठी है। पढ़ना-लिखना भी हुआ कहाँ। गरीब विधवा की संतान, चाचा के घर पली-बढ़ी। अपने दो-दो भतीजों को पढ़ाने-लिखाने में ही चाचा की नाक में दम तो भतीजी को पढ़ाने का सवाल ही कहाँ !
फीस के पैसे जमा नहीं हो सके मैट्रिक की पूरी परीक्षा भी न दे सकी सुलेखा। उसके बाद तो ईश्वर की अपार अनुकंपा से ब्याह हो गया। शक्ल-सूरत अच्छी थी, इसलिए कृपा करना भी आसान हो गया। अत¬¬ शिक्षा का प्रसार स्कूल की चारदीवारी तक ही रह गया।
मगर निशीथ रंजन तो पड़ा-लिखा युवक था। खैर, उसकी बात जाने दें। अब तो सुलेखा एड़ी-चोटी एक कर गृहस्थी की टूटी नाव को खींच-खींचकर किनारे के करीब आ ही चुकी है। अब अगर इंतजार है तो इस बात का कि नाव पर सवार लोग छलाँग भरकर किनारे उतर पड़ें और अपने-अपने रास्ते निकल जाएँ। अब आकर बीते हुए अनेक वर्षों की मूर्खता का हिसाब लगाना भी निरर्थक ही होगा।
और भी निरर्थक होगा-कौन अधिक मूर्ख था-इस बात पर तर्क उठाना ।
अब तो सबकुछ सुंदर है, सजा-सँवरा है। अब अगर बच्चों के बारे में कोई पूछताछ करे तो आराम से कहा जा सकता है-दो बेटे, तीन बेटियाँ हैं-बड़ा बेटा मेड़िकल स्टुडेंट है, अगले वर्ष फाइनल परीक्षा देगा। बड़ी बेटी ने बी.ए. पासकर बी.टी. पढ़ना आरंभ किया है। मझली बेटी बी.एस.सी. में पढ़ रही है, छोटी ने इस बार हायर सेंकेडरी की परीक्षा दी है और सबसे छोटा बेटा दसवीं कक्षा में है।
सुलझा हुआ परिवार है, जैसे मोहरे बिछाए हुए शतरंज की बिसात हो। बस, खेल शुरू करने भर की देर है।
मगर हैरत की बात तो यह है कि अब अक्सर सुलेखा को लगता है कि खेलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं लगता है कि ये पाँचों बच्चे जब छोटे थे, तभी जीवन और सरल था।
तब झंझट होता भी था तो उन्हें नहलाने-खिलानें में, उनके कपड़े और गुदड़ी बदलने में, उनकी जिद पूरी करने में हरदम निगरानी करने में। कोई खाट से गिर न जाए, कोई सड़क पर निकल न जाए। और क्या था ? और तो कुछ याद नहीं आता। फिर पता नहीं क्यों, सुलेखा दिन-रात सोचा करती थी।–उफ, ये किसी तरह बड़े हो जाएँ तो मैं चैन की साँस ले सकूँ।
क्या पाँचों की पाँच किस्म की जरूरतें होती थीं, इसीलिए ?
तब तो दो बच्चे दोपहर में स्कूल जाने लगे थे, बाकी तीनों सवेरे। उन्हें दस बजे के भीतर ही नहला-खिलाकर भेजना पड़ता था, इन दोनों को भी उसी समय तैयार कर देती थी। पहले इन्हें देखे या फिर उनके लिए चावल पकाने बैठे, समझ नहीं पाती थी वह। घर के प्रधान सदस्य को तो ठीक नौ बजे खाना तैयार चाहिए।
तब सुलेखा को लगता था कि पानी में कूदें या आग में ? कभी तो सोचती थी-उफ, ये बड़े-बड़े हो जाएँ किसी तरह।....सुबह के काम से निपटते ही सुबह के स्कूल से बच्चे वापस आ जाते थे। तब उन्हें पकड़कर नहला-खिलाकर सुलाना-मल्ल-युद्ध से कम था क्या ? अकसर सुलाने की वह कोशिश भी बेकार जाती थी। सुलेखा न सो पाती थी, न कुछ काम कर पाती थी। कहानी की किताब पढ़ना ? वह तो सपना था।
मगर किताब पढ़ने की कितनी चाहत थी उसमें। वैसे, उसी में जीवन का सही अर्थ मिल जाता था।
इसके लिए उसकी चेष्टाओं का अंत नहीं था, अंत नहीं था डाँट खाने का भी। फिर भी नशा छूटता नहीं था।
हाथ में कहानी की किताब देखते ही चाची बोल उठती थीं, ‘यह किताब फिर कहाँ से आ गई ?’
चाची बेजार होकर कहती थीं, ‘घर में एक लाइब्रेरी से तो किताबें आती ही रही हैं। फिर भी इसके घर, उसके घर जाकर किताब माँगकर लाना। पता नहीं ऐसा भी क्या नशा है ! क्यों ? मुझे भी तो कहानी-उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्या मैं मुहल्ले में घूम-घूमकर माँगती फिरती हूँ ? किताब लाइब्रेरी से मँगाकर पढ़ी जाती है, यही तो जानती हूँ।’
चाची तो केवल इतना जानती हैं, यह सुलेखा को अच्छी तरह मालूम है और यह भी जानती है कि चाची की धारणा से पसंद की चीज का आनंद धीरे-धीरे लेना चाहिए।
अत: लाइब्रेरी से किताब बदलकर ले आना महीने में कुल तीन-चार बार ही होता होगा। अगर किताब मोटी हुई तो और भी कम।
तो फिर ? सुलेखा के मन की भूख मिटाने के लिए महीने में सिर्फ दो-तीन पुस्तकें ? घर-घर से मँगवाकर लाए बिना चारा ही क्या ?
पाँच दिन भोजन किए बिना पड़ी रह सकती है सुलेखा आराम से, परन्तु पाँच दिन किताब के बिना ? वैसा जीवन तो मरुभूमि-सा ही कठिन और नीरस होगा।
अत: निरुपाय सुलेखा प्यास बुझाने की आस लेकर पड़ोस के घर जाकर पूछती है, ‘नीला चाची, आपने लाइब्रेरी से किताब बदली क्या ?’.....किसी और के घर जाकर कहती, ‘मौसीजी, फिर आ गई आपको परेशान करने। उस दिन विभूति बंदोपाध्याय की जो किताब पढ़ रही थी, पूरा पढ़ लिया क्या ?’......नहीं तो कभी मोड़ पर जाकर सामने वाले घर में सावधानी से पूछती है, ‘समीर चाचा घर पर हैं ?’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i