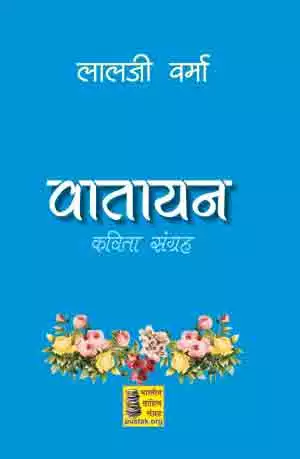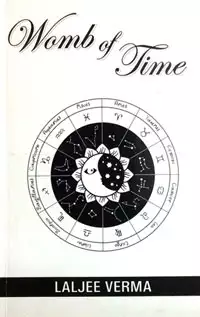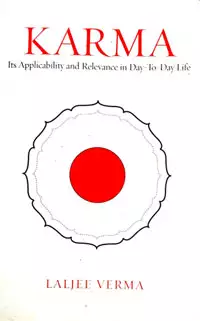|
नई पुस्तकें >> वातायन वातायनलालजी वर्मा
|
|
|||||||||
लालजी वर्मा की कविताएँ
गूगल बुक्स में प्रिव्यू के लिए क्लिक करें
सदा से यह प्रश्न उठता आया है कि साहित्य है क्या? साहित्य पनपता क्यों है? किसी समय-विशेष में एक खास तरह का साहित्य पनपता है। तो क्या अलग-अलग समाज में अलग-अलग साहित्य का परिचय होता है? नहीं, मैं नहीं मानता कि साहित्य अलग-अलग होता है। साहित्य तो समाज का दर्पण होता है। किसी भी समाज-विशेष से संबंध उसका अवश्य होता है, पर मूलत: एक ही बात तो प्रत्येक साहित्य में मिलती है, और वह है समाज की अच्छाइयां, बुराइयां, कठिनाइयां और आकांक्षाएं। साहित्य को दिशा नहीं चाहिए क्योंकि इसमें दिशा तो सहज निहित है। साहित्य को जबरदस्ती दिशा देने वाले लोग साहित्य के प्रति केवल अन्याय ही नहीं करते बल्कि अपने दायित्व से भी च्युत होते हैं।
तो प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी कुछ, जो लिखा जाता है, साहित्य है? कदापि नहीं। साहित्य में धारा चाहिए और उसके लिए भाषा की आवश्यकता है। साहित्य में आलोचक, समालोचक और प्रकाशक का भी अपना ही स्थान है। हां, आलोचना आज समझने-समझाने के लिए करें तो और भी रचनात्मक होगा। प्रकाशकों की अवस्था तो गोताखोर की तरह होती है। जो समुद्र में गोते लगाकर ज्यादा मोती ऊपर लाने में सफल हुआ वह अच्छा गोताखोर कहलाएगा। पर एक बात यहां सोचने को विवश कर देती है—क्या मोती वही नहीं जो सतह पर लाया गया? वैसे तो सागर-गर्भ में अनगिनत मोती हैं; पर उससे क्या?
आजकल कविता का प्रकाशन अवगुंठन में पड़ा है। प्रकाशकों से पूछने पर वे यह नहीं कहते कि आपकी रचना योग्य नहीं है। पर यह कहते हैं कि यह शैली मेरे काम की नहीं। कुछ ऐसा दबाव है कि केवल आधुनिक कविता या हास्य-कविता ही छपती है। खैर, ऐसे में पारिजात प्रकाशन का और श्री शंकरदयाल सिंह के सहयोग और सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार का मैं बराबर आभारी बना रहूंगा।
मेरा यह कहना नहीं है कि प्रकाशक अपने व्यवसाय में ऊँच-नीच का भेद न करें, पर प्रकाशन में रूढ़िवाद साहित्य को कमजोर बना देता है। साहित्य में दिशा और धारा दोनों ही आवश्यक हैं। हां, यहां मैं यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि यह बातें साहित्यिक होने की हैसियत से नहीं बल्कि पाठक की हैसियत से कह रहा हूँ।
लेकिन प्रश्न उठता है कि साहित्य का छपना क्यों लेखक के लिए आवश्यक है? मेरी समझ से छपने से और पाठकों के सामने पहुंचने से लेखक को बढ़ावा मिलता है और लिखने की क्रिया को एक धारा मिलती आजकल के समाज में विरोधाभास काफी प्रबल है। सभी तरफ 'मुंह में राम, बगल में छुरी' की कहावत चरितार्थ हो रही है। मानव-मूल्यों का ह्रास हो रहा है, भौतिकवाद हमारे जीवन में कूट-कूटकर भर गया है। और यह जानते हए भी कि भौतिकवाद किसी के हित में नहीं है—न तो अपने हित में और न समाज के हित में - सभी उसी विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यह कहाँ का विधान है, समझ में नहीं आता। हम करना कुछ चाहते हैं पर करते कुछ और ही हैं। समाज और जन-जीवन सभी इसी रोग से ग्रस्त हैं। ऐसा लगता है, कोई दानव या जिन्न हम सबों को अपनी तरफ खींच रहा है और हम सभी बस विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
'था पथिक पिये जीवन-मदिरा, सोता-जागता चलता जाता'
शायद कलियुग इसे ही कहते हैं ! यहां विनाश से मेरा अभिप्राय प्रलय से नहीं अपितु मानव और समाज के मूल्यों के विनाश से है। और जब सामाजिक तत्व का विघटन होगा, जब मनुष्य इकाई की, परिवार की, संबंधों की कोई कद्र नहीं करेगा, तो कैसा होगा वह समाज, यह सोचकर ही सिहरन होती है, दहशत होती है। वही प्रलय होगा। अच्छाइयों और बुराइयों के बीच युद्ध। विजय किसकी होगी? विवेक कहता है विजय अच्छाइयों की होगी। पर कितनी पीडा के बाद, कितने तपन के बाद! और अगर यह कल्पना सही नहीं उतरती तो फिर शायद कभी भी मानवसमाज की आधारशिला नहीं बनेगी। कोई मानव नहीं रहेगा। रहेंगे केवल पशु !
प्रलय के बाद समाज-निर्माण फिर नये सिरे से शुरू होगा। फिर नये-नये विधाता, ईश्वर, खुदा बनाए जाएंगे, फिर समाज का विकास इनको केंद्र-बिंदु मानकर किया जाएगा। और फिर विरोध, विनाश और फिर निर्माण। शायद जीव-जगत का चक्र है। बार-बार हम उसी समय को लांघकर आगे निकल रहे हैं। लोग कहते हैं, 'समय बीत गया, समय तेजी से निकलता है, जाड़े की रात - समय काटते नहीं कटता' इत्यादि। पर क्या यह सच नहीं कि समय स्वयं द्वार बन खड़ा है, हम लोग ही बार-बार आ-जा रहे हैं?
सूरज तो रोज ही निकलता है, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती रहती है, सूर्य अपनी जगह है, पर शायद पूरा सौर मंडल वृहद आकाश में अपनी निर्धारित धुरी पर घूम रहा है। मनुष्य-जीवन की तुलना में ये सभी स्थिर ही हैं और हमारे लिए समय वही है। हम लोग ही जन्म लेते हैं, क्रमश: आयु बढ़ती है और अंतत: हम मौत के घाट लग जाते हैं। फिर पुनर्जन्म और फिर वही गति-विधि।
'है समय खड़ा बस एक ठौर, हम-तुम ही आते-जाते हैं।'
समय शायद एक बिंदु है और स्रष्टा की सारी रचना उसी के चारों ओर घूम रही है। सच पूछा जाए तो जीवन का हर पहलू वृत्ताकार है, चन्द्रमा पृथ्वी के, पृथ्वी सूर्य के और सौरमंडल ब्रह्मांड में किसी अज्ञात केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। आत्मा जीव में, काया में बंधकर परमात्मा के चारों ओर घूमती रहती है और जन्म और पुनर्जन्म का क्रम चलता रहता है। आत्मा का विलय परमात्मा में मोक्ष मिलने पर होता है। जब तक केंद्र में आकर्षण की शक्ति है तब तक परिधि पर काया और आत्मा का गमन होगा। जब काया के तत्व का विनाश होगा तभी
आत्मा आकर्षण से परे हो जाएगी। जीवन में विरोधाभास है। ईश्वर का अस्तित्व सृष्टि में है पर सृष्टि है इसीलिए तो ईश्वर की कल्पना है, मानता हूँ कि तुमसे ही मेरी अस्मिता है, पर यह भी तो सत्य है कि मैं हूँ इसीलिए तुम्हारी भी अस्मिता है। सौंदर्य का आभास केवल फूल पर ही निर्भर नहीं, उसके सौंदर्य को देखने, परखने और अभिव्यक्त करने पर है। पर यहां सौंदर्य फूल पर भी तो निर्भर है। अनुभूति और अभिव्यक्ति मानव के विवेक के दो अभिन्न अंग हैं। अभिव्यक्ति की आधारशिला अनुभूति पर है और अनुभूति जब तक व्यक्त न की जाय, सिसकती राख-सी अपनी आंतरिक आंच को प्रकट किए बिना ही बुझकर रह जाती है। कोई भी दो मनुष्य एक तरह की अनुभूति नहीं रखते — चाहे वे एक ही वातावरण में क्यों न पले हों। इसलिए सबके विचार अलग-अलग होते हैं। किसी भी चीज को, भाव को, या सृष्टि को देखने के लिए आंखें वहीं रहते हुए भी मन रूपी कंप्यूटर पर जो इंप्रिंट पड़ता है वह अलग-अलग रहता है। मनुष्य-मनुष्य में इसीलिए विरोधाभास है और बराबर रहेगा।
मैंने इस पुस्तक का संकलन करने में बहुत समय लिया है। इसमें दी गई रचनाएं 1975 से 1984 तक की हैं। इसे पाठकों के समीप लाने का श्रेय श्री शंकरदयाल सिंह का है, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। एतद् संबंधी सुधार-सुझाव के लिए मैं श्री अमरेश कुमार पांडेय का आभारी हूँ।
साहित्य, जग-बीती और आपबीती का समन्वय है, जहाँ साहित्य का ज्वार-भाटा उठता है। साहित्य, जन-जीवन, समाज और जीव-जगत की ऊर्जा से उठता स्पंदन है। मैंने यही समझकर इन कविताओं की रचना की है। इन्हें इसी संदर्भ में पढ़ा और परखा जाए, यही मेरी कामना, मेरी प्रार्थना है।
- लालजी वर्म
|
|||||


 i
i