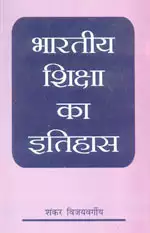|
भाषा एवं साहित्य >> भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय शिक्षा का इतिहासशंकर विजयवर्गीय
|
114 पाठक हैं |
|||||||
शिक्षकों, शिक्षण-संस्थाओं और शिक्षाविदों के लिए अत्यन्त उपयोगी संदर्भ-ग्रन्थ।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
शिक्षा-नीति शिक्षण-कला आदि विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं परन्तु
भारत में शिक्षा के इतिहास पर सम्भवतः यह पहली प्रामाणिक पुस्तक है
विद्वान लेखक ने वर्षों के परिश्रम से भारतीय शिक्षा की विकास-यात्रा का
सर्वांगीण इतिवृत्त प्रस्तुत किया है। वेदकालीन शिक्षाप्रणाली से लेकर
अधुनातन खुले विद्यालयों नवोदय स्कूलों और दूरस्थ शिक्षाप्रणाली की विशद्
विवेचना की है और इक्कीसवीं सदी में आनेवाली शिक्षा समस्याओं पर
विचार-विमर्श भी। समय-समय पर सरकार द्वारा तथा विभिन्न शिक्षा-आयोगों
द्वारा जो नीतिगत परिवर्तन हुए उनकी सार्थकता, व्यावहारिकता एवं सफलता को
भी जाँचा-परखा है।
शिक्षकों, शिक्षण-संस्थाओं और शिक्षाविदों के लिए अत्यन्त उपयोगी संदर्भ-ग्रन्थ।
शिक्षकों, शिक्षण-संस्थाओं और शिक्षाविदों के लिए अत्यन्त उपयोगी संदर्भ-ग्रन्थ।
निवेदन
भारतीय शिक्षा के इतिहास की एक झलक हिन्दी पाठकों की सेवा में प्रस्तुत
है। शिक्षा का इतिहास प्राय: शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उपयोग की
दृष्टि से लिखा गया है; किन्तु यह तो एक अत्यन्त ही सीमित पाठक वृंद हैं।
प्रस्तुत पुस्तक के लेखन में सामान्य हिन्दी पाठक को भी ध्यान में रखा गया
है। विचार यह रहा है कि भारतीय नागरिक भी अपनी शिक्षा के विभिन्न युगों और
इनमें शिक्षा की प्रगति से परिचित हो सके। आशा है इस दृष्टि से पुस्तक
उपयोगी सिद्ध होगी।
इस पुस्तक में शिक्षा के इतिहास के अतिरिक्त शिक्षा की अद्यतन प्रगति पर प्रकाश डालने वाले अंश भी सम्मिलित हैं। वर्तमान की शिक्षा समस्याओं पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के अत्यन्त ही बृहत प्रतिवेदन को केवल कुछ पृष्ठों में समेटने का प्रयास भी है। अन्त में यह प्रश्न भी उठाया गया है कि बीसवीं सदी के इक्कीसवीं सदी से जोड़ने वाले इस दसवें दशक में किन समस्याओं से जूझना होगा।
इस पुस्तक में भारतीय शिक्षा की एक संक्षिप्त झलक है। उम्मीद है कि पुस्तक हिन्दी पाठकों को रुचिकर लगेगी।
इस पुस्तक के लेखन में लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यकार और मेरे अभिन्न मित्र ‘वीणा’ सम्पादक प्रोफेसर डा. श्याम सुन्दर व्यास की प्रेरणा फलदायी हुई है। लेकिन उनके प्रति आभार प्रकट करना निरी धृष्टता होगी।
इस पुस्तक में शिक्षा के इतिहास के अतिरिक्त शिक्षा की अद्यतन प्रगति पर प्रकाश डालने वाले अंश भी सम्मिलित हैं। वर्तमान की शिक्षा समस्याओं पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के अत्यन्त ही बृहत प्रतिवेदन को केवल कुछ पृष्ठों में समेटने का प्रयास भी है। अन्त में यह प्रश्न भी उठाया गया है कि बीसवीं सदी के इक्कीसवीं सदी से जोड़ने वाले इस दसवें दशक में किन समस्याओं से जूझना होगा।
इस पुस्तक में भारतीय शिक्षा की एक संक्षिप्त झलक है। उम्मीद है कि पुस्तक हिन्दी पाठकों को रुचिकर लगेगी।
इस पुस्तक के लेखन में लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यकार और मेरे अभिन्न मित्र ‘वीणा’ सम्पादक प्रोफेसर डा. श्याम सुन्दर व्यास की प्रेरणा फलदायी हुई है। लेकिन उनके प्रति आभार प्रकट करना निरी धृष्टता होगी।
शंकर विजयवर्गीय
1
प्राचीन भारतीय शिक्षा-दर्शन
जीवन-दर्शन और शिक्षा-दर्शन के मध्य वैषम्य की कोई कल्पना नहीं की जा सकती
है। वे एक-दूसरे के पूरक हैं और एक-दूसरे को प्रभावित भी करते हैं।
जीवन-दर्शन की दृष्टि से प्राचीन भारतीय दर्शन के विभिन्न कालों के बीच
गहरी रेखायें नहीं खींची जा सकती हैं। प्राचीन भारत की संस्कृति शाश्वत और
सतत् रही है, अविभाज्य रही है। विद्वानों ने वैदिक संस्कृति से महाकाव्य
(रामायण और महाभारत) कालीन संस्कृति में प्राथक्य स्थापित करने के प्रयत्न
किये हैं; किन्तु बाद वाले काल में भी वैदिक संस्कृति और जीवन शैली का
स्पष्ट प्रभाव है; साम्य भी है। वैदिक जीवन शैली महाकाव्यकालीन जीवन शैली
में प्राचुर्य है। यह सत्य है कि रामायण और महाभारत में वर्णित कुछ जीवन
पद्धतियाँ वैदिक काल में नहीं हैं। अत: वेदकालीन जीवन-दर्शन का अस्तित्व
पृथक से स्वीकार किया जा सकता है। इसी तारतम्य में यदि हम महाकाव्यकालीन
युग का पृथक अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं तब भी वैदिक संस्कारों का युग
में भी विद्यमान होना स्वीकार करना ही होगा।
इस परिप्रेक्ष्य में प्राचीन भारत के इतिहास को एक इकाई के रूप में होना चाहिए। इसी तारतम्य में प्राचीन भारतीय शिक्षा-दर्शन को भी सर्वप्रथम एक इकाई के रूप में ही मान्य किया जाना चाहिए। यह हो सकता है कि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने के लिए उपर्युक्त दोनों युगों की सीमायें निर्धारित की जायें किन्तु विशेषकर बाद वाले युग में प्रथम युग की इतनी अधिक विशेषतायें विद्यमान हैं कि दोनों युगों के जीवन-दर्शन और शिक्षा-दर्शन पर एक साथ विचार करना भी उपयोगी होगा।
प्राचीन भारतीय जीवन-दर्शन धर्ममय था। जीवन के सभी कार्यकलाप धर्म से ओत-प्रोत थे, धर्म से नियंत्रित थे। धर्म द्वारा, धर्म के लिए और धर्ममय जीवन शैली प्राचीन भारत की विशेषता थी। वर्तमान जीवन में राजनीति का प्रभुत्व है। धर्म, समाज, अर्थ आदि सभी में राजनीति का प्रवेश है। सभी पर राजनीति हावी है। प्राचीन युग की प्रधानता होने से राजनीति में हिंसा और शत्रुता, द्वेष और ईर्ष्या, परिग्रह और स्वार्थ का बहुल्य न होकर, प्रेम, सदाचार त्याग और अपरिग्रह महत्वपूर्ण थे। उदात्त भावनायें बलवती थीं। दिव्य सिद्धान्त जीवन के मार्गदर्शक थे। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति प्रधान नहीं था, अपितु वह परिवार और समाज के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करने को तत्पर था। उदात्त वृत्ति की सीमा सम्पूर्ण वसुधा थी। जीवन का आदर्श ‘वसुधैवकुटुम्बकम्’ था। जीवन का उद्देश्य धर्म था। धर्ममय जीवन भौतिक उपलब्धियों से श्रेष्ठ माना जाता था।
प्राचीन भारत का शिक्षा-दर्शन भी धर्म से ही प्रभावित था। शिक्षा का उद्देश्य धर्माचरण की वृत्ति जाग्रत करना था। शिक्षा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए थी। इनका क्रमिक विकास ही शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य था। धर्म का सर्वप्रथम स्थान था। धर्म से विपरीत होकर अर्थ लाभ करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध करना था। मोक्ष जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य था और यही शिक्षा का भी अन्तिम लक्ष्य था। प्राचीन काल में जीवन-दर्शन ने शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया था। जीवन की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का प्रभाव शिक्षा दर्शन पर भी पड़ा था। उस काल के शिक्षकों, ऋषियों आदि ने चित्त-वृत्ति-निरोध को शिक्षा का उद्देश्य माना था। शिक्षा का लक्ष्य यह भी था कि आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। उस समय भौतिक सुविधाओं के विकास की ओर ध्यान देना किंचित भी आवश्यक नहीं था क्योंकि भूमि धन-धान्य से पूर्ण थी, भूमि पर जनसंख्या का भार नहीं था। किन्तु इसका यह भी अर्थ नहीं था कि लोकोपयोगी शिक्षा का आभाव था। प्रथमत: लोकोपयोगी शिक्षा परिवार में, परिवार के मध्यम से ही सम्पन्न हो जाती थीं। वंश की परंपरायें थीं और ये परम्परायें पिता से पुत्र को हस्तान्तरित होती रहती थीं। व्यवसायों के क्षेत्र में प्रतियोगिता नहीं के बराबर थीं। सभी के लिए काम उपलब्ध था। सभी की आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती थीं।
चाहे वैदिक युग में हो अथवा महाकाव्य काल में हो, प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति में ऋषिगण समाज के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। वे सभी शिक्षक के समधर्मी थे। वे सदा ही आध्यात्मिक सत्ता के गुण गाते थे। उनका जीवन भौतिकता से मुक्त और आध्यात्मिकता में लिप्त रहता था। समाज को भी वे यही शिक्षा और मार्गदर्शन देते थे। वैदिक काल से प्रारम्भ होकर, महाकाव्य काल में यह जीवन-दर्शन परवान चढ़ा। इस प्रकार प्राचीन काल में भारतीय जीवन-दर्शन पूर्णत: आध्यात्मिक रहा और शिक्षा को भी यही दिशा मिली। गुरु परंपरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही। वेदों का प्रादुर्भाव भी गुरु परंपरा से ही हुआ। तत्पश्चात भी शिक्षा गुरु परम्परा के माध्यम से ही दी जाती रही।
यद्यपि व्यवसायों का शिक्षण अधिकतर गृह प्रांगण में ही होता था किन्तु गुरु-गृह भी गृहस्थी की शिक्षा के समुन्नत केन्द्र थे। भारत उस काल में भी कृषि प्रधान देश था। कृषि, वनोपज और पशुपालन का शिक्षण प्राय: गुरु-गृह में निवास कर प्राप्त होता था। मानव प्रकृति की गोद से दूर नहीं रहता था। गुरु-गृह अधिकतर बस्तियों से दूर रहते थे। उनमें रहने वाले विद्याभ्यामी प्रकृति के प्रांगण में निवास करते थे, विचरते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे और अभ्यास एवं अनुप्रयोग करते थे। चाहे धनवान-पुत्र हो या निर्धन-पुत्र, कृषि कार्य एवं वनवास और वनविचरण के कार्यों एवं प्रवृत्तियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों ही वर्ग के शिष्यों के लिए ऐसे कार्यों द्वारा श्रम का गौरव आत्मसात करना और व्यवहार में लाना उपयोगी माना जाता था। श्रम का गौरव समाज में पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित और महिमा मण्डित था। इसके अतिरिक्त सेवा-कार्य को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। गुरु-गृह में गुरु, गुरु-परिवार तथा सहपाठियों की सेवा को उत्कृष्ठ कार्य माना जाता था। गुरु की गायों की सेवा भी शिष्य का कर्त्तव्य था। गुरुकुल में मानवोपयोगी पशुओं की संख्या सैकड़ों और हजारों में होती थी।
सामूहिकता का अत्याधिक महत्व था। गुरु सैकड़ों की संख्या में गौपालन इसलिए नहीं करता था कि उसे निजी लाभ हो और उसका परिवार भौतिक सुविधायें भोग सके अपितु इस उद्यम का लाभ गुरुकुल में निवास करने वाले सभी शिष्य आदिवासियों को मिलता था। छान्दोग्य उपनिषद् में महासन्त सत्यकाम की कथा का वर्णन है। प्रारम्भ में तो वे गुरु की गौवों की रक्षा में रत रहते थे बाद में उनकी देख-रेख में सहस्त्र गायों का पालन करते थे। विभिन्न प्रकार के दानों में गौदान का सार्वाधिक महत्व था। गौदान को स्वर्णदान से भी अधिक महान माना जाता था। शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था में गोधन सर्वोपरि था। गृहस्थाश्रम के लिए उपयुक्त इस शिक्षा की पृष्ठभूमि में वही सिद्धान्त था जिसको वर्तमान में हम ‘क्रिया से शिक्षा’ की संज्ञा देते हैं। उच्चतम शिक्षा में भी ‘शारीरिक श्रम’ और ‘क्रिया’ का अत्याधिक महत्व था। आध्यात्मिक उन्नति में संलग्न ऋषि एवं शिष्य भी शारीरिक श्रम से दूर नहीं रहते थे।
इसका यही अर्थ है कि शिक्षा केवल सैद्धान्तिक नहीं थी। व्यवहार और वास्तविकता का भी शिक्षा से उतना ही गहन संबंध था जितना सैद्धांतिक अध्ययन-अध्यापन का। किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझा जाता था। ऋग्वेद में ऐसे उदाहरण हैं कि ऋषि स्वयं कवि थे, उनके पिता चिकित्सक थे, उनकी माता उपल प्रक्षिणी अर्थात् आटा पीसने वाली थी और परिवार के तीनों ही सदस्य शिक्षा दान में कार्यरत थे।
क्रिया द्वारा शिक्षा के लिए जीवन एक प्रयोगशाला के समान था। ऋषि कुल में जीवनयापन के मध्य शिक्षा संबंधी प्रयोग और परीक्षण सम्पन्न होते थे। इन प्रयोगों के आधार पर ही शिक्षाशास्त्र विकसित हुआ था। यहाँ तक शिक्षण विधि का प्रश्न है, श्रवण, मनन और चिंतन, प्रयोग और व्यवहार को समुचित स्थान प्राप्त था। स्मरण शक्ति का यथोचित उपयोग किया जाता था। गुरु परंपरा का महत्व भी अत्यधिक था। यह गुरु परंपरा की ही देन है कि वेद आज तक जीवित हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा का विकास, आध्यात्मिकता, चित्त-वृत्ति-निरोध, लोकोपयोग, गृहस्थ-जीवन-प्रशिक्षण, श्रम की पूजा, कृषि का प्रायोगिक ज्ञान आदि को सम्मिलित कर हुआ था।
ऋषिकुल अथवा गुरुकुल में निवास करने वाले किसी भी शिष्य या उसके परिवार से शुल्क लेने की प्रथा नहीं थी। प्राय: वे आश्रम आत्म-निर्भर होते थे। पशुपालन या कृषि उत्पादन से इन आश्रमों या गुरुकुल का सम्पूर्ण व्यय वहन होता था। अनेक आश्रम ऐसे भी थे जिनके लिए इस प्रकार से व्यय पूर्ति संभव नहीं थी। उनके लिए भिक्षा प्राप्त करने का उपाय था। शिष्यगण और स्वयं गुरु भी भिक्षा माँगने को अधम अथवा हीन नहीं मानते थे। भिक्षा स्वयं माँगने वाले के लिए नहीं होकर समूह के लिए होती थी। वे भिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की लज्जा या ग्लानि का अनुभव नहीं करते थे। निर्धन और धनिक दोनों ही प्रकार के परिवारों से आये शिष्य भिक्षा प्राप्ति में समान रूप से भाग लेते थे। ‘एक सब के लिए और सब एक के लिए’ वाले सिद्धान्त पर सम्पूर्ण व्यवस्था आधारित थी।
गुरु भी भिक्षा माँगने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। भिक्षा उनके स्वयं के उदर पोषण या भौतिक सुविधाओं के लिए नहीं होती थी अपितु आश्रम के संचालन और विकास के लिए वे राजा या धनिकों के द्वार पर दान प्राप्त करने के लिए भिक्षु के रूप में उपस्थित होते थे। वे दान में गौएं और स्वर्ण प्राप्त करते थे। जब शिष्य अपने ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर अपने परिवार में पहुँचते थे और गृहस्थ का जीवन अपनाते थे तब उन्हें इस भिक्षा की वृत्ति की उपादेयता ज्ञात रहती थी। उनके पास उनका स्वयं का अनुभव होता था कि किस प्रकार उनके शिष्य काल में प्राप्त भिक्षा सर्वाहिताय होती थी। अत: वे मुक्त हृदय से दान देने में पीछे नहीं रहते थे।
ऋषि की ख्याति के अनुरूप आश्रम चयन की सुविधा शिष्य के परिवार को रहती थी किन्तु आश्रम, धनवानों के आश्रम और निर्धनों के आश्रम में बंटे नहीं थे। आश्रम में सभी स्तर के शिष्य एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। राजा और रंक में किसी प्रकार का भेद नहीं था। सभी एक साथ गुरु की छत्र-छाया में निवास करते थे, विद्याभ्यास करते थे। महाकाव्य काल में संपादिनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा राजपुत्र और रंक-पुत्र के एक साथ शिक्षा प्राप्त करने और जीवनपर्यन्त मित्रता निभाने का उदाहरण स्मरणीय है।
गुरु का महत्व अत्यधिक था। शिक्षा, शिल्प-केन्द्रित थी। ऋषियों के अपने आश्रम थे। आश्रम उनके ही नाम से विख्यात थे। उनके स्थान निश्चित थे। गुरु परंपरा में एक पीढ़ी के पश्चात् दूसरी पीढ़ी आती रहती थी।
इस परिप्रेक्ष्य में प्राचीन भारत के इतिहास को एक इकाई के रूप में होना चाहिए। इसी तारतम्य में प्राचीन भारतीय शिक्षा-दर्शन को भी सर्वप्रथम एक इकाई के रूप में ही मान्य किया जाना चाहिए। यह हो सकता है कि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने के लिए उपर्युक्त दोनों युगों की सीमायें निर्धारित की जायें किन्तु विशेषकर बाद वाले युग में प्रथम युग की इतनी अधिक विशेषतायें विद्यमान हैं कि दोनों युगों के जीवन-दर्शन और शिक्षा-दर्शन पर एक साथ विचार करना भी उपयोगी होगा।
प्राचीन भारतीय जीवन-दर्शन धर्ममय था। जीवन के सभी कार्यकलाप धर्म से ओत-प्रोत थे, धर्म से नियंत्रित थे। धर्म द्वारा, धर्म के लिए और धर्ममय जीवन शैली प्राचीन भारत की विशेषता थी। वर्तमान जीवन में राजनीति का प्रभुत्व है। धर्म, समाज, अर्थ आदि सभी में राजनीति का प्रवेश है। सभी पर राजनीति हावी है। प्राचीन युग की प्रधानता होने से राजनीति में हिंसा और शत्रुता, द्वेष और ईर्ष्या, परिग्रह और स्वार्थ का बहुल्य न होकर, प्रेम, सदाचार त्याग और अपरिग्रह महत्वपूर्ण थे। उदात्त भावनायें बलवती थीं। दिव्य सिद्धान्त जीवन के मार्गदर्शक थे। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति प्रधान नहीं था, अपितु वह परिवार और समाज के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करने को तत्पर था। उदात्त वृत्ति की सीमा सम्पूर्ण वसुधा थी। जीवन का आदर्श ‘वसुधैवकुटुम्बकम्’ था। जीवन का उद्देश्य धर्म था। धर्ममय जीवन भौतिक उपलब्धियों से श्रेष्ठ माना जाता था।
प्राचीन भारत का शिक्षा-दर्शन भी धर्म से ही प्रभावित था। शिक्षा का उद्देश्य धर्माचरण की वृत्ति जाग्रत करना था। शिक्षा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए थी। इनका क्रमिक विकास ही शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य था। धर्म का सर्वप्रथम स्थान था। धर्म से विपरीत होकर अर्थ लाभ करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध करना था। मोक्ष जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य था और यही शिक्षा का भी अन्तिम लक्ष्य था। प्राचीन काल में जीवन-दर्शन ने शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया था। जीवन की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का प्रभाव शिक्षा दर्शन पर भी पड़ा था। उस काल के शिक्षकों, ऋषियों आदि ने चित्त-वृत्ति-निरोध को शिक्षा का उद्देश्य माना था। शिक्षा का लक्ष्य यह भी था कि आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। उस समय भौतिक सुविधाओं के विकास की ओर ध्यान देना किंचित भी आवश्यक नहीं था क्योंकि भूमि धन-धान्य से पूर्ण थी, भूमि पर जनसंख्या का भार नहीं था। किन्तु इसका यह भी अर्थ नहीं था कि लोकोपयोगी शिक्षा का आभाव था। प्रथमत: लोकोपयोगी शिक्षा परिवार में, परिवार के मध्यम से ही सम्पन्न हो जाती थीं। वंश की परंपरायें थीं और ये परम्परायें पिता से पुत्र को हस्तान्तरित होती रहती थीं। व्यवसायों के क्षेत्र में प्रतियोगिता नहीं के बराबर थीं। सभी के लिए काम उपलब्ध था। सभी की आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती थीं।
चाहे वैदिक युग में हो अथवा महाकाव्य काल में हो, प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति में ऋषिगण समाज के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। वे सभी शिक्षक के समधर्मी थे। वे सदा ही आध्यात्मिक सत्ता के गुण गाते थे। उनका जीवन भौतिकता से मुक्त और आध्यात्मिकता में लिप्त रहता था। समाज को भी वे यही शिक्षा और मार्गदर्शन देते थे। वैदिक काल से प्रारम्भ होकर, महाकाव्य काल में यह जीवन-दर्शन परवान चढ़ा। इस प्रकार प्राचीन काल में भारतीय जीवन-दर्शन पूर्णत: आध्यात्मिक रहा और शिक्षा को भी यही दिशा मिली। गुरु परंपरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही। वेदों का प्रादुर्भाव भी गुरु परंपरा से ही हुआ। तत्पश्चात भी शिक्षा गुरु परम्परा के माध्यम से ही दी जाती रही।
यद्यपि व्यवसायों का शिक्षण अधिकतर गृह प्रांगण में ही होता था किन्तु गुरु-गृह भी गृहस्थी की शिक्षा के समुन्नत केन्द्र थे। भारत उस काल में भी कृषि प्रधान देश था। कृषि, वनोपज और पशुपालन का शिक्षण प्राय: गुरु-गृह में निवास कर प्राप्त होता था। मानव प्रकृति की गोद से दूर नहीं रहता था। गुरु-गृह अधिकतर बस्तियों से दूर रहते थे। उनमें रहने वाले विद्याभ्यामी प्रकृति के प्रांगण में निवास करते थे, विचरते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे और अभ्यास एवं अनुप्रयोग करते थे। चाहे धनवान-पुत्र हो या निर्धन-पुत्र, कृषि कार्य एवं वनवास और वनविचरण के कार्यों एवं प्रवृत्तियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों ही वर्ग के शिष्यों के लिए ऐसे कार्यों द्वारा श्रम का गौरव आत्मसात करना और व्यवहार में लाना उपयोगी माना जाता था। श्रम का गौरव समाज में पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित और महिमा मण्डित था। इसके अतिरिक्त सेवा-कार्य को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। गुरु-गृह में गुरु, गुरु-परिवार तथा सहपाठियों की सेवा को उत्कृष्ठ कार्य माना जाता था। गुरु की गायों की सेवा भी शिष्य का कर्त्तव्य था। गुरुकुल में मानवोपयोगी पशुओं की संख्या सैकड़ों और हजारों में होती थी।
सामूहिकता का अत्याधिक महत्व था। गुरु सैकड़ों की संख्या में गौपालन इसलिए नहीं करता था कि उसे निजी लाभ हो और उसका परिवार भौतिक सुविधायें भोग सके अपितु इस उद्यम का लाभ गुरुकुल में निवास करने वाले सभी शिष्य आदिवासियों को मिलता था। छान्दोग्य उपनिषद् में महासन्त सत्यकाम की कथा का वर्णन है। प्रारम्भ में तो वे गुरु की गौवों की रक्षा में रत रहते थे बाद में उनकी देख-रेख में सहस्त्र गायों का पालन करते थे। विभिन्न प्रकार के दानों में गौदान का सार्वाधिक महत्व था। गौदान को स्वर्णदान से भी अधिक महान माना जाता था। शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था में गोधन सर्वोपरि था। गृहस्थाश्रम के लिए उपयुक्त इस शिक्षा की पृष्ठभूमि में वही सिद्धान्त था जिसको वर्तमान में हम ‘क्रिया से शिक्षा’ की संज्ञा देते हैं। उच्चतम शिक्षा में भी ‘शारीरिक श्रम’ और ‘क्रिया’ का अत्याधिक महत्व था। आध्यात्मिक उन्नति में संलग्न ऋषि एवं शिष्य भी शारीरिक श्रम से दूर नहीं रहते थे।
इसका यही अर्थ है कि शिक्षा केवल सैद्धान्तिक नहीं थी। व्यवहार और वास्तविकता का भी शिक्षा से उतना ही गहन संबंध था जितना सैद्धांतिक अध्ययन-अध्यापन का। किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझा जाता था। ऋग्वेद में ऐसे उदाहरण हैं कि ऋषि स्वयं कवि थे, उनके पिता चिकित्सक थे, उनकी माता उपल प्रक्षिणी अर्थात् आटा पीसने वाली थी और परिवार के तीनों ही सदस्य शिक्षा दान में कार्यरत थे।
क्रिया द्वारा शिक्षा के लिए जीवन एक प्रयोगशाला के समान था। ऋषि कुल में जीवनयापन के मध्य शिक्षा संबंधी प्रयोग और परीक्षण सम्पन्न होते थे। इन प्रयोगों के आधार पर ही शिक्षाशास्त्र विकसित हुआ था। यहाँ तक शिक्षण विधि का प्रश्न है, श्रवण, मनन और चिंतन, प्रयोग और व्यवहार को समुचित स्थान प्राप्त था। स्मरण शक्ति का यथोचित उपयोग किया जाता था। गुरु परंपरा का महत्व भी अत्यधिक था। यह गुरु परंपरा की ही देन है कि वेद आज तक जीवित हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा का विकास, आध्यात्मिकता, चित्त-वृत्ति-निरोध, लोकोपयोग, गृहस्थ-जीवन-प्रशिक्षण, श्रम की पूजा, कृषि का प्रायोगिक ज्ञान आदि को सम्मिलित कर हुआ था।
ऋषिकुल अथवा गुरुकुल में निवास करने वाले किसी भी शिष्य या उसके परिवार से शुल्क लेने की प्रथा नहीं थी। प्राय: वे आश्रम आत्म-निर्भर होते थे। पशुपालन या कृषि उत्पादन से इन आश्रमों या गुरुकुल का सम्पूर्ण व्यय वहन होता था। अनेक आश्रम ऐसे भी थे जिनके लिए इस प्रकार से व्यय पूर्ति संभव नहीं थी। उनके लिए भिक्षा प्राप्त करने का उपाय था। शिष्यगण और स्वयं गुरु भी भिक्षा माँगने को अधम अथवा हीन नहीं मानते थे। भिक्षा स्वयं माँगने वाले के लिए नहीं होकर समूह के लिए होती थी। वे भिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की लज्जा या ग्लानि का अनुभव नहीं करते थे। निर्धन और धनिक दोनों ही प्रकार के परिवारों से आये शिष्य भिक्षा प्राप्ति में समान रूप से भाग लेते थे। ‘एक सब के लिए और सब एक के लिए’ वाले सिद्धान्त पर सम्पूर्ण व्यवस्था आधारित थी।
गुरु भी भिक्षा माँगने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। भिक्षा उनके स्वयं के उदर पोषण या भौतिक सुविधाओं के लिए नहीं होती थी अपितु आश्रम के संचालन और विकास के लिए वे राजा या धनिकों के द्वार पर दान प्राप्त करने के लिए भिक्षु के रूप में उपस्थित होते थे। वे दान में गौएं और स्वर्ण प्राप्त करते थे। जब शिष्य अपने ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर अपने परिवार में पहुँचते थे और गृहस्थ का जीवन अपनाते थे तब उन्हें इस भिक्षा की वृत्ति की उपादेयता ज्ञात रहती थी। उनके पास उनका स्वयं का अनुभव होता था कि किस प्रकार उनके शिष्य काल में प्राप्त भिक्षा सर्वाहिताय होती थी। अत: वे मुक्त हृदय से दान देने में पीछे नहीं रहते थे।
ऋषि की ख्याति के अनुरूप आश्रम चयन की सुविधा शिष्य के परिवार को रहती थी किन्तु आश्रम, धनवानों के आश्रम और निर्धनों के आश्रम में बंटे नहीं थे। आश्रम में सभी स्तर के शिष्य एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। राजा और रंक में किसी प्रकार का भेद नहीं था। सभी एक साथ गुरु की छत्र-छाया में निवास करते थे, विद्याभ्यास करते थे। महाकाव्य काल में संपादिनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा राजपुत्र और रंक-पुत्र के एक साथ शिक्षा प्राप्त करने और जीवनपर्यन्त मित्रता निभाने का उदाहरण स्मरणीय है।
गुरु का महत्व अत्यधिक था। शिक्षा, शिल्प-केन्द्रित थी। ऋषियों के अपने आश्रम थे। आश्रम उनके ही नाम से विख्यात थे। उनके स्थान निश्चित थे। गुरु परंपरा में एक पीढ़ी के पश्चात् दूसरी पीढ़ी आती रहती थी।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i