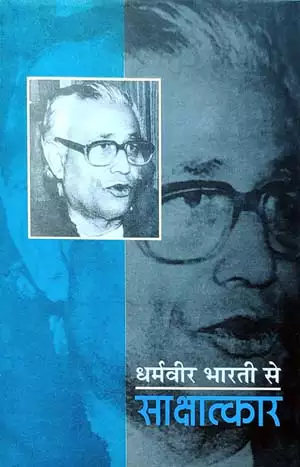|
संस्मरण >> धर्मवीर भारती से साक्षात्कार धर्मवीर भारती से साक्षात्कारपुष्पा भारती
|
114 पाठक हैं |
|||||||
अपने समय के एक शीर्षस्थ कवि, चिन्तक, साहित्यकार और पत्रकार धर्मवीर भारती के बहुरंगी और बहुआयामी साक्षात्कार...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
साहित्य में सम्मान और लोकप्रियता के शिखर पर प्रतिष्ठित और नयी हिन्दी
पत्रकारिता के महत्त्वपूर्ण स्तम्भ डॉ. धर्मवीर भारती से किये गये
साक्षात्कारों की यह विशिष्ट कृति हैं ‘धर्मवीर भारती से
साक्षात्कार’।
इसमें अपने समय के एक शीर्षस्थ कवि, चिन्तक, साहित्यकार और पत्रकार धर्मवीर भारती के बहुरंगी और बहुआयामी साक्षात्कार हैं; जिनके माध्यम से उनके अन्तरंग यथार्थ, उनका प्रखर चिन्तन और उनकी सर्जनात्मक वैचारिकता मुखर हैं।
कह सकते हैं यह पुस्तक भारती जी के जीवन और कर्म का जीवन्त दस्तावेज है। इसमें खट्टी-मीठी बहुत-सी यादों, बहुत सी अनुभूतियों और राग-विराग जीवन-संघर्ष तथा समस्याओं से जुड़े अनेक बेलौस प्रश्नों के बेबाक उत्तर भारती जी ने दिये हैं।
‘धर्मवीर से साक्षात्कार’ में एक ओर जहाँ भारती जी की सांस्कृतिक मूल्यों, जीवन और समाज की जटिलताओं मौजूदा विकास और वैचारिक रुगण्ता को देखने-समझने की दृष्टि उजागर है वहीं इसमें अनेक इतिहास बोध और संस्कार आध्यात्मिक संघर्ष और द्वन्द्व की विकलता तथा साहित्य परिदृश्य के सम्बन्ध में उनके विचारों से भी साक्षात्कार होता है।
हिन्दी साहित्य के सुधी पाठकों के लिए एक अनिवार्य पुस्तक।
इसमें अपने समय के एक शीर्षस्थ कवि, चिन्तक, साहित्यकार और पत्रकार धर्मवीर भारती के बहुरंगी और बहुआयामी साक्षात्कार हैं; जिनके माध्यम से उनके अन्तरंग यथार्थ, उनका प्रखर चिन्तन और उनकी सर्जनात्मक वैचारिकता मुखर हैं।
कह सकते हैं यह पुस्तक भारती जी के जीवन और कर्म का जीवन्त दस्तावेज है। इसमें खट्टी-मीठी बहुत-सी यादों, बहुत सी अनुभूतियों और राग-विराग जीवन-संघर्ष तथा समस्याओं से जुड़े अनेक बेलौस प्रश्नों के बेबाक उत्तर भारती जी ने दिये हैं।
‘धर्मवीर से साक्षात्कार’ में एक ओर जहाँ भारती जी की सांस्कृतिक मूल्यों, जीवन और समाज की जटिलताओं मौजूदा विकास और वैचारिक रुगण्ता को देखने-समझने की दृष्टि उजागर है वहीं इसमें अनेक इतिहास बोध और संस्कार आध्यात्मिक संघर्ष और द्वन्द्व की विकलता तथा साहित्य परिदृश्य के सम्बन्ध में उनके विचारों से भी साक्षात्कार होता है।
हिन्दी साहित्य के सुधी पाठकों के लिए एक अनिवार्य पुस्तक।
भूमिका
विश्व की सभी भाषाओं में महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के साक्षात्कार लेने की
प्रथा खासी पुरानी है। हिन्दी में इधर यह कुछ ज्यादा ही प्रचलित हो गयी
है। शायद है कि प्रच्छन्न कारण मीडिया का प्रसार हो। अब लिखित शब्द पढ़ने
की फुर्सत लोगों में कम रह गयी है। पर बहुत कुछ जानने और समझने की तलब भी
बढ़ गयी है। उस सिलसिले में साक्षात्कार पढ़कर सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति
के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में काफी-कुछ जान लेने का सन्तोष मिल
जाता है। इसीलिए साक्षात्कारों का रिवाज इतना बढ़ गया है। पर इसमें एक
गड़बड़ यह हो जाती है कि साक्षात्कार छोटी-बड़ी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं
में छपकर गुम हो जाते हैं, उनका केवल तात्कालिक उपयोग मात्र हो पाता है।
भारतीजी की एक विशेष आदत थी कि वह जो कुछ भी करते थे पूरे मनोयोग से करते थे। पूरी ईमानदारी से करने की गुंजाइश जिस काम में नहीं होती थी उस काम को वह करते ही नहीं थे। साक्षात्कार उन्होंने अधिक नहीं दिये, पर जो दिये पूरे मन से और गम्भीरता से दिये-साक्षात्कारकर्ता को यों ही टरका देने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। मैं जितने भी आलेख उपलब्ध कर सकी उन्हें संकलित करके भारतीजी को प्रेम करनेवाले असंख्य पाठकों को सौंप रही हूँ-इन्हें पढ़कर आप उन्हें और करीब से तथा पारदर्शी ढंग से जान सकेंगे। साथ ही एक बहुत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भी आपको भेंट करती हूँ जो भारतीजी ने स्वयं अपने हाथों लिखा है। मुझे पता नहीं यह पत्र किस शोध-छात्र के लिए कब लिखा गया था। उनके यत्र-तत्र बिखरे कागजों को सँभालते-सहेजते समय यह कागज मिले-मैं खुद चमत्कृत रह गयी कि उन्होंने अपना आत्मपरिचय स्वयं लिखा ! क्योंकि उनके सहमते-संकोची स्वभाव से मैं परिचित हूँ। वह केवल अपना काम करते रहना पसन्द करते थे। अपने बारे में कभी बढ़-चढ़कर कुछ बोलने, करने की यहाँ तक कि सुनने की भी उनकी आदत ही नहीं थी, आत्म-प्रशंसा की बात तो छोड़िए, सामान्य तथ्य भी वो बताने से कतराते रहते थे। इस आलेख में तो उन्होंने अपने पूरे जीवन की यात्रा के महत्त्वपूर्ण पड़ावों का जिक्र खुद ही कर दिया है। यह जिक्र डॉ. भारती से आपका सीधा साक्षात्कार करा रहा है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं।
इन साक्षात्कारों को प्रस्तुत करनेवाले सभी लेखकों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। निश्चय ही वे भी भारतीजी को फिर इस तरह जानना और याद किया जाना पसन्द करेंगे। भारती जन्म-दिवस 25 दिसम्बर, 1998
भारतीजी की एक विशेष आदत थी कि वह जो कुछ भी करते थे पूरे मनोयोग से करते थे। पूरी ईमानदारी से करने की गुंजाइश जिस काम में नहीं होती थी उस काम को वह करते ही नहीं थे। साक्षात्कार उन्होंने अधिक नहीं दिये, पर जो दिये पूरे मन से और गम्भीरता से दिये-साक्षात्कारकर्ता को यों ही टरका देने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। मैं जितने भी आलेख उपलब्ध कर सकी उन्हें संकलित करके भारतीजी को प्रेम करनेवाले असंख्य पाठकों को सौंप रही हूँ-इन्हें पढ़कर आप उन्हें और करीब से तथा पारदर्शी ढंग से जान सकेंगे। साथ ही एक बहुत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भी आपको भेंट करती हूँ जो भारतीजी ने स्वयं अपने हाथों लिखा है। मुझे पता नहीं यह पत्र किस शोध-छात्र के लिए कब लिखा गया था। उनके यत्र-तत्र बिखरे कागजों को सँभालते-सहेजते समय यह कागज मिले-मैं खुद चमत्कृत रह गयी कि उन्होंने अपना आत्मपरिचय स्वयं लिखा ! क्योंकि उनके सहमते-संकोची स्वभाव से मैं परिचित हूँ। वह केवल अपना काम करते रहना पसन्द करते थे। अपने बारे में कभी बढ़-चढ़कर कुछ बोलने, करने की यहाँ तक कि सुनने की भी उनकी आदत ही नहीं थी, आत्म-प्रशंसा की बात तो छोड़िए, सामान्य तथ्य भी वो बताने से कतराते रहते थे। इस आलेख में तो उन्होंने अपने पूरे जीवन की यात्रा के महत्त्वपूर्ण पड़ावों का जिक्र खुद ही कर दिया है। यह जिक्र डॉ. भारती से आपका सीधा साक्षात्कार करा रहा है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं।
इन साक्षात्कारों को प्रस्तुत करनेवाले सभी लेखकों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। निश्चय ही वे भी भारतीजी को फिर इस तरह जानना और याद किया जाना पसन्द करेंगे। भारती जन्म-दिवस 25 दिसम्बर, 1998
पुष्पा भारती
भारतीजी का एक पत्र
[भारतीजी ने यह पत्र कब किसके लिए लिखा था, कोशिशों के बावजूद इसकी
जानकारी नहीं मिल सकी है। बहरहाल अब यह उनके असंख्य पाठकों के लिए यहाँ
प्रस्तुत है-एक अद्वितीय सामग्री के रूप में।]
प्रिय भाई,
मुझे बहुत खेद है कि आपके अनेक पत्र मिले पर यथासमय न तो मैं उनके उत्तर दे सका न आपको उसके लिए आवश्यक सामग्री ही भेज सका। इसका मुख्य कारण यही है कि मुझे अपने बारे में कुछ भी लिखने या बात करने में बहुत संकोच महसूस होता है। यह मेरा स्वभाव है। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि मैंने अपने बारे में कहीं कुछ भी लिखा हो।
फिर भी चूँकि आपकी थीसिस के लिए आवश्यक है अत: संक्षेप में अपने जीवन और उस पर पड़े प्रभावों की रूपरेखा लिख रहा हूँ। अनेक मामलों में तिथियाँ मुझे याद नहीं है, जो याद है वह लिख दूँगा। मेरा जन्म 25 दिसम्बर 1926 को इलाहाबाद के अतरसुइया मुहल्ले के मकान में हुआ। मेरे पिता का नाम श्री चिरंजीवलाल वर्मा और माता का नाम श्रीमती चन्दा देवी था। परिवार का इतिहास यह था कि हमारा वंश मूलत: शाहजहाँपुर जिले (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) के ख़ुदागंज नाम के कस्बे का निवासी था। वहाँ हम लोगों की बहुत बड़ी जमींदारी थी। खेत और अनेक आम के बगीचे। एक बहुत बड़ी कोठी कुछ पक्की कुछ कच्ची। मेरे बाबा का नाम एवज राय था। वे एक धनी दबंग जमींदार थे और उनके साथ एक व्यक्ति सदैव बन्दूक लेकर चलता था। मैं बहुत बचपन में छुट्टियों में माता-पिता के साथ ख़ुदागंज जाया करता था और तब की अनेक यादें अभी भी सजीव हैं। उस कोठी में तीन आँगन थे और कोठी के अन्दर ही दो कुएँ थे। मरदाने, आँगन के पास एक बड़ा कमरा था जिसमें बन्दूकें तलवारें, बरछियाँ लाठियाँ लालटेनें, मशालें रखी रहती थीं और दीवार पर दो जिरह-बख्तर और एक ढाल टँगी रहती थी। कटारें और बघनखे भी ताख में रखे रहते थे। यह नहीं मालूम कि यह बाबा एवज राय का शौक था या मेरे ताऊ अशर्फीलाल का, जो बाबा के मरने के बाद घर के बुजुर्ग थे।
बहरहाल वह कमरा मेरे कुतूहल का विशेष केन्द्र था, और जब भी छुट्टियों में ख़ुदागंज जाता तब मेरे आकर्षण के दो ही केन्द्र होते-कोठी के पिछवाड़े के विशाल आँगन में लगी मेहँदी, आम, इमली, बेला, गुलतस्वी के झाड़ और तरह-तरह की फूलवाली लतरें, उनमें उड़ते तोते और आँगन में खेलते गाय के बछड़े। फूलों, रंगों और खुशुबुओं से प्यार इसी आँगन से पनपा। और दूसरा केन्द्र था वह कमरा तलवारों और बरछियोंवाला जहाँ अकसर बैठकर नौकरों से डकैतों और परियों की कहानियाँ सुनता, ‘बालसखा’ या बच्चों की आयी पत्रिकाएँ पढ़ता। कभी-कभी मेरा नौकर ‘खूबी’ मुझे कुरते-धोती पर कमरबन्ध बाँधकर कमर में एक मखमली म्यान की कटार खोंस देता और मैं उसी धज में पड़ोस के पण्डिती के घर या सामने के शिवाले में घूमता रहता। पड़ोस के पण्डित चाचा संस्कृत के विद्वान थे और मेरे पिता के अच्छे मित्र थे। उनकी विशेषता यह थी कि वे प्रात:काल स्नान के समय कोई स्तोत्र या श्लोक आदि न पढ़कर सस्वर ‘गीतगोविन्द’ का पाठ करते थे। माँ उनकी इस आदत पर अप्रसन्न होतीं पर पिता अकसर उनसे ‘गीतगोविन्द’ सुनते। मेरी दोपहरें अकसर सामने के शिव-मन्दिर में बीततीं। वह पुराना मन्दिर शाम और सुबह तो आरती-पूजा के कारण भीड़-भरा रहता व दोपहर को सुनसान। उस समय उसके ठण्डे पत्थर के फर्श पर लेटे रहना मुझे बहुत पसन्द था। छत से बूँद-बूँद जो पानी चूता वह तटहटी तक पहुंचते-पहुंचते गुलाब की खुशबू में बस जाता। उस पानी से मैं गरमी की दोपहर भर मुँह पर छींटे देता रहता।
मेरे पिता पाँच भाई थे। दो वहीं रहते थे। तीन अन्य नगरों में। सभी अपने परिवार सहित ख़ुदागंज में इकट्ठे होते। सोने से लदी, बहुत बूढ़ी दादी अपनी अँधेरी कोठरी में पलंग पर लेटी रहतीं और बारी-बारी से बेटों और बहुओं से खुश या नाराज होती रहतीं। मुझे उस कोठरी में जाने का एक ही लालच था कि वे बड़े घड़े में से निकालकर सोंठ की कतली या मूँग के लड्डू देतीं। पर वैसे वे मुझे बहुत पसन्द नहीं थी।
मुझे अच्छी लगती थी ‘अइया’। वे किसी रिश्तेदार ताऊ की विधवा पत्नी थीं, जिनका गुजर-बसर का कोई दूसरा जरिया नहीं था, अत: वे हमारे परिवार की आश्रिता थीं। तड़के सुबह उठकर आँगन की कुइयाँ से पानी भरना, बरतन माँजना, चौका लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, दादी के पाँव दबाना, सुबह चार बजे से रात दस बजे तक वे मशीन की तरह खटती थीं। सब बहुएँ उनके पाँव तो छूती थीं पर उन्हें नौकरानी की तरह झिड़कती भी थीं।
‘बालसखा’ में परियों की कहानी पढ़-पढ़कर कई बार मैं सोचता कि अइया श्रापग्रस्त रानी है। मैं उनको बहुत चाहता था। उन्हीं के कामकाज में हाथ बँटाता रहता और जब फुरसत मिलती तो उनके साथ छत की दीवार पर बैठकर बातें करता। वे गाँव की नाइनों, धोबिनों, भठियारिनों और डकैतों की घरवालियों के किस्से मुझे सुनातीं और मैं उन्हें अपने भूगोल की कक्षा में पढ़े हुए पाठ-समुद्र क्या होता है, बादल कैसे बनते हैं, यू.पी. में आकर वे कैसे बरसते हैं, हॉलैण्ड के बच्चे काठ के जूते पहनते हैं और एस्किमो बारहसिंगा का दूध पीते हैं-ये कथाएँ सुनाया करता था। मेरी आधी झूठी आधी सच्ची कहानियों की सबसे पहली प्रशंसक अइया थी। एक बार तेज बुखार आया और अइया चल बसीं।
हम लोगों का ख़ुदागंज जाना भी छूट गया। उसका कारण यह था कि मेरे पिता एक प्रकार से अपने परिवार की सामन्ती जमींदारी परम्परा के विद्रोही थे। बाबा और ताऊ चाहते थे कि वे लगान वसूली और लेन-देन का काम सँभाले, लेकिन मेरे पिता छुटपन में ही बरेली चले गये। कुछ पढ़-लिखकर रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में ओवरसीयरी का इम्तहान पास कर आये। बाबा ने मारे गुस्से के बहुत-कुछ सख्त सुस्त कहा तो घर छोड़कर जंगलात के टीले की किसी फर्म में ओवरसीयर होकर बर्मा चले गये और वहाँ सागौन के जंगलों में भटकते रहे। वहाँ से काफी रुपया कमाकर लाये तो मीरजापुर में बसे, वहाँ आटे की चक्की और आटे की मिलें लगायीं पर उनमें नुकसान हुआ और जाने कैसे इलाहाबाद आ बसे। वहाँ अतरसुइया मुहल्ले में मकान बनाया। यह सब मेरे इस संसार में आने के पहले की बातें हैं।
मैंने होश संभाला तो अतरसुइया की गली और माँ-बाप के आर्य-समाजी वातावरण में। माँ कट्टर आर्य-समाजी थीं। मेरे जन्म के पहले मेरे 10 भाई-बहन पैदा होकर मर चुके थे, अत: वे हमेशा मुझे साथ रखतीं। सन्ध्या, हवन, जनेऊ, ब्रह्मचर्य सभी विधिवत्। पिता समझदार आर्य-समाजी थे। वे मुझे हर तरह की किताबें पढ़ने को देते जिनसे माँ परहेज करती थीं। चन्द्रकान्ता सन्तति, भूतनाथ, रक्त मण्डल, चाँद का फाँसी अंक, भारत में अँग्रेजी राज, महात्मा गाँधी की आत्मकथा और चन्द्रशेखर आजाद और भगतसिंह की जीवनियाँ। उस समय का प्रखर तेजस्वी पत्र ‘भविष्य’ हमारे घर नियमित आता था। ख़ुदागंज में कमरबन्द में कटार खोंसकर चलनेवाला बच्चा अब चन्द्रशेखर आजाद की तरह पिस्तौल बाँधकर चलने या ‘रक्त मण्डल’ की तरह अँग्रजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति करने का स्वप्न देखने लगा था।
एक बार ख़ुदागंज से चिट्ठी आयी। ताऊ अशर्फीलाल का देहावसान हो गया था और सबसे छोटे चाचा जमीन-जायदाद का बँटवारा करना चाहते थे। पिता अकेले गये। लौट कर आये तो बहुत थके टूटे-से दिख रहे थे। माँ को उन्होंने जो बताया वह मैंने दरवाजे के पास से सुना। जिन भाइयों को उन्होंने बच्चों की तरह पाला-पोसा और लिखाया-पढ़ाया, नौकरी दिलायी, वे सब इनके खून के प्यासे हो उठे थे। कारण यह था कि जायदाद के हिस्से के अलावा, दादी ने अपने पुराने गहने इन्हें अलग से दे दिये थे। जीवन-भर के विद्रोही बच्चे के प्रति दादी अकस्मात् ममतामयी हो उठी थीं। खूब झगड़े और गाली-गलौज के बाद जीवन-भर ख़ुदागंज न लौटने का प्रण कर वे अन्तिम बार घर को विदा देके चले। बिस्तरा, टीन का ट्रंक और गहने साथ थे। वहाँ से स्टेशन मीरनपुर 12-13 मील दूर है। बैलगाड़ी से जाना होता था। रास्ते में रात हुई और नहर के पासवाले आम के बगीचे में लठैतों ने हमला बोल दिया। ये गहने लेकर एक आम के पेड़ पर चढ़कर छिपकर बैठे रहे। रात-भर लठैत ढूंढ़ते रहे और रात-भर ये छिपे रहे। सुबह होने पर उतरे। असबाब तो लुट चुका था। पोटली लिए स्टेशन पहुंचे। मुँह-हाथ धोकर सन्ध्या की, गायत्री का जाप किया और एक परिचित बूढ़े गाड़ीवाले को गहने की पोटली दी कि दादी को लौटा दे और गहने दूसरे भाइयों की बहुओं को बाँट दिये जाएँ-और चले आये। नमक रोटी कमाएँगे और उसमें खुश रहेंगे।
मैंने उस दिन दरवाजे के पास से यह वृत्तान्त सुना और पिता का भक्त हो गया। उनके मूल्य, उनकी प्रखरता, उनकी उदार दृष्टि, उनकी देश-भक्ति, उनकी समझौता-विहीन ईमानदारी मेरा आदर्श बन गयी...
और फिर आये चरम गरीबी के दिन। पहले पिता ने एक नौकरी स्वीकार की और आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन के नोटिफाइड एरिया के दप्तर में ओवरसीयर हो गये। मेरे बचपन के दो वर्ष मऊनाथ भंजन में बीते। यह सन् 32 का जमाना रहा होगा। उन्हीं दिनों गाँधीजी ने इक्कीस दिन का उपवास किया था। पिता खद्दर और चर्खे के बजाय आजाद और भगतसिंह के प्रशंसक थे, पर उन इक्कीस दिनों में उन्होने एक वक्त खाना नहीं खाया। अन्त में गाँधीजी की पुकार पर सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर इलाहाबाद लौट आये।
और अब शुरू हुए भयंकर गरीबी के दुर्दिन !
पिता कुछ ठेकेदारों वगैरह के लिए नक्शे-वक्शे बनाने का काम करते रहते पर उससे पूरा नहीं पड़ता था। मां के बचे-खुचे गहने वगैरह बेचकर, कुछ कर्ज वगैरह लेकर उन्होंने दो मकान और बनवाये कि ये कुछ काम आएँगे। उसी बीच में माँ सख्त बीमार पड़ गयी और दो साल तक बीमार रहीं। बीमारी की फिक्र और कर्ज की फ्रिक ने पिता को मन और शरीर से तोड़ दिया, पिता सख्त बीमार पड़े और शायद नवम्बर 1939 में उनकी मृत्यु हो गयी। तब मैं 13 वर्ष का था और 8वीं या 9वें दर्जे में था।
उन भयानक दिनों में हमारे दूर के रिश्ते के मामा श्री अभयकृष्ण चौधरी ने बहुत सहायता की। कर्ज उतराने और गुजर-बसर करने के लिए माँ छोटी बहन को लेकर गुरुकुल में नौकरी करने चली गयीं और मैं मामा के पास रहा। मामी ने माँ से बढ़कर स्नेह दिया और मामा ने संरक्षक और अमिट ममता दी, और मैं खूब पढ़ूँ-लिखूँ और कुछ बड़ा काम करूँ-इसकी प्रेरणा वे बराबर मन में भरते रहे। 42 के आन्दोलन में मैंने भाग लिया और सुभाष का बड़ा प्रशंसक बना, और वजीफों तथा मामा की सहायता से पढ़ता रहा। पाठ्य-पुस्तकों के अलावा कविता पुस्तकें तथा अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ने का बेहद शौक रहा और उसी से लेखन के बीज मन में पड़े। उन्हीं दिनों मैंने शेले, कीट्स, वर्डस्वर्थ, टेनीसन, एमिली डिकिन्सन तथा अनेक फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश कवियों को अँग्रेजी अनुवाद में पढ़ा। एमिल ज़ोला, शरतचन्द्र, गोर्की, कुप्रिन, बालज़क, डिकेन्स, विक्टर ह्यूगो, दास्तावस्की तथा तॉल्स्तॉय के उपन्यास पढ़े। तॉल्स्तॉय का ‘वार ऐण्ड पीस’ मेरे जीवन पर स्थायी प्रभाव छोड़ गया।
बी.ए. और एम.ए. की पढ़ाई ट्यूशनों के सहारे चली। कुछ दिन ‘अभ्युदय’ ‘संगम’ और हिन्दुस्तानी एकेडेमी में काम किया। उसी समय ‘मुर्दों का गाँव‘, ‘पृथ्वी और स्वर्ग’ दो कहानी-संग्रह छपे। प्रारम्भिक। उस समय मुझ पर जयशंकर प्रसाद और ऑस्कर वाइल्ड का बहुत प्रभाव था। तभी मैं माखनलाल चतुर्वेदी के सम्पर्क में आया, उन्होंने लिखने को बहुत प्रोत्साहित किया।
एम.ए. कर लेने के बाद मार्क्सवाद का अध्ययन प्रारम्भ किया। प्रगतिशील लेखक संघ का स्थानीय मन्त्री भी रहा कुछ दिन, पर कम्युनिस्टों की कट्टरता तथा देशद्रोही नीतियों से मोहभंग हुआ। तभी मैंने छहों भारतीय दर्शन, वेदान्त तथा विस्तार से वैष्णव और सन्त साहित्य पढ़ा और भारतीय चिन्तन की मानववादी परम्परा मेरे चिन्तन का मूल आधार बन गयी। उन्हीं दिनों पहले ‘गुनाहों का देवता’, फिर ‘प्रगतिवाद एक समीक्षा’ तथा ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा।’ लिखा।
कविता के क्षेत्र में मुझे छायावादी भाषा के बजाय बच्चन, नेपाली, नरेन्द्र शर्मा की काव्यभाषा अधिक ग्राह्य लगी तथा शेले, कीट्स और ऑस्कर वाइल्ड का प्रारम्भिक प्रभाव काव्य-शैली पर रहा। उसी समय ‘अज्ञेय’ से भेंट हुई और ‘अज्ञेय’ ने कुछ कविताएँ ‘दूसरा सप्तक’ के लिए चुनीं। उसके बाद ‘ठण्डा लोहा’ प्रकाशित हुआ।
माँ जरा कट्टर किस्म की आर्य-समाजी थीं। उन्हें यह साहित्यिक लेखन और जीवन बहुत पसन्द नहीं था पर मामा ने बहुत प्रोत्साहन दिया। उस समय तक ‘परिमल’ संस्था काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। मैं उसके प्रारम्भिक सदस्यों में था। मतवाद के घेरे में साहित्य को बाँधना ठीक नहीं है इस बात को लेकर प्रगतिशील लेखकों से काफी विवाद रहता था। तभी नवलेखन के प्रतिनिधि त्रैमासिक के रूप में ‘निकष’ का प्रकाशन शुरू किया। उसी समय ‘नदी प्यासी थी’, ‘चाँद और टूटे हुए लोग’, ‘ठेले पर हिमालय’, ‘सिद्ध साहित्य’ का प्रकाशन हुआ। तब मैं विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगा था। इस दौरान अस्तित्ववादी तथा पश्चिम के अन्य नये दर्शनों का विशिष्ट अध्ययन किया। रिल्के के कविताएँ, कामू के लेख और नाटक, ज्याँ पॉल सार्त्र की रचनाएँ और कार्ल मार्क्स की दार्शनिक रचनाओं में काफी डूबा और साथ ही महाभारत, गीता, विनोबा और लोहिया के साहित्य का विशेष अध्ययन किया। गाँधीजी को भी नये परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की। भारतीय सन्त और सूफी-काव्य विशेषत: कबीर, जायसी और सूर को पुन: पढ़ा और समझा। नाथ परम्परा और सिद्ध साहित्य तो रिसर्च के विषय थे ही।
सन् ’55 के आसपास एक पंजाबी शरणार्थी लड़की से विवाह हुआ। संस्कारों के तीव्र वैषम्य के कारण वह विवाह असफल रहा और बाद में विच्छेद हो गया।
सन् ’60 में बम्बई आ गया। उसके पहले ‘सात गीत वर्ष’, ‘अन्धा युग’, ‘कनुप्रिया’, ‘देशान्तर’ प्रकाशित हो चुके थे। बम्बई आने के बाद ‘बन्द गली का आखिरी मकान’, ‘कहनी अनकहनी’, ‘पश्यन्ती’ प्रकाशित हुए। पुष्पा भारती से विवाह हुआ, जिसने बहुत सुख, सन्तोष और शान्ति दी। केवल जीवन में नहीं वरन् विचारों और साहित्य-चिन्तन के क्षेत्र में भी उनका एक सार्थक गहरा, प्रेरणाप्रद साथ मिला।
इधर पत्रकारिता की व्यस्तता के कारण लिखने का उतना समय नहीं मिल पाता है। कुछ जो लिखा वह छपाया नहीं है।
संक्षेप में जीवन और साहित्यिक प्रगति की यह रूपरेखा है। कैशोर्य तथा ‘परिमल’ युग और बाद में बम्बई जीवन की भी बहुत सी उल्लेखनीय बातें हैं, पर उन सबको लिखूँगा तो पूरी पुस्तक हो जाएगी। अत: इतनी सूचना भेज रहा हूँ जिससे आपका इस समय काम चल जाए।
प्रिय भाई,
मुझे बहुत खेद है कि आपके अनेक पत्र मिले पर यथासमय न तो मैं उनके उत्तर दे सका न आपको उसके लिए आवश्यक सामग्री ही भेज सका। इसका मुख्य कारण यही है कि मुझे अपने बारे में कुछ भी लिखने या बात करने में बहुत संकोच महसूस होता है। यह मेरा स्वभाव है। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि मैंने अपने बारे में कहीं कुछ भी लिखा हो।
फिर भी चूँकि आपकी थीसिस के लिए आवश्यक है अत: संक्षेप में अपने जीवन और उस पर पड़े प्रभावों की रूपरेखा लिख रहा हूँ। अनेक मामलों में तिथियाँ मुझे याद नहीं है, जो याद है वह लिख दूँगा। मेरा जन्म 25 दिसम्बर 1926 को इलाहाबाद के अतरसुइया मुहल्ले के मकान में हुआ। मेरे पिता का नाम श्री चिरंजीवलाल वर्मा और माता का नाम श्रीमती चन्दा देवी था। परिवार का इतिहास यह था कि हमारा वंश मूलत: शाहजहाँपुर जिले (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) के ख़ुदागंज नाम के कस्बे का निवासी था। वहाँ हम लोगों की बहुत बड़ी जमींदारी थी। खेत और अनेक आम के बगीचे। एक बहुत बड़ी कोठी कुछ पक्की कुछ कच्ची। मेरे बाबा का नाम एवज राय था। वे एक धनी दबंग जमींदार थे और उनके साथ एक व्यक्ति सदैव बन्दूक लेकर चलता था। मैं बहुत बचपन में छुट्टियों में माता-पिता के साथ ख़ुदागंज जाया करता था और तब की अनेक यादें अभी भी सजीव हैं। उस कोठी में तीन आँगन थे और कोठी के अन्दर ही दो कुएँ थे। मरदाने, आँगन के पास एक बड़ा कमरा था जिसमें बन्दूकें तलवारें, बरछियाँ लाठियाँ लालटेनें, मशालें रखी रहती थीं और दीवार पर दो जिरह-बख्तर और एक ढाल टँगी रहती थी। कटारें और बघनखे भी ताख में रखे रहते थे। यह नहीं मालूम कि यह बाबा एवज राय का शौक था या मेरे ताऊ अशर्फीलाल का, जो बाबा के मरने के बाद घर के बुजुर्ग थे।
बहरहाल वह कमरा मेरे कुतूहल का विशेष केन्द्र था, और जब भी छुट्टियों में ख़ुदागंज जाता तब मेरे आकर्षण के दो ही केन्द्र होते-कोठी के पिछवाड़े के विशाल आँगन में लगी मेहँदी, आम, इमली, बेला, गुलतस्वी के झाड़ और तरह-तरह की फूलवाली लतरें, उनमें उड़ते तोते और आँगन में खेलते गाय के बछड़े। फूलों, रंगों और खुशुबुओं से प्यार इसी आँगन से पनपा। और दूसरा केन्द्र था वह कमरा तलवारों और बरछियोंवाला जहाँ अकसर बैठकर नौकरों से डकैतों और परियों की कहानियाँ सुनता, ‘बालसखा’ या बच्चों की आयी पत्रिकाएँ पढ़ता। कभी-कभी मेरा नौकर ‘खूबी’ मुझे कुरते-धोती पर कमरबन्ध बाँधकर कमर में एक मखमली म्यान की कटार खोंस देता और मैं उसी धज में पड़ोस के पण्डिती के घर या सामने के शिवाले में घूमता रहता। पड़ोस के पण्डित चाचा संस्कृत के विद्वान थे और मेरे पिता के अच्छे मित्र थे। उनकी विशेषता यह थी कि वे प्रात:काल स्नान के समय कोई स्तोत्र या श्लोक आदि न पढ़कर सस्वर ‘गीतगोविन्द’ का पाठ करते थे। माँ उनकी इस आदत पर अप्रसन्न होतीं पर पिता अकसर उनसे ‘गीतगोविन्द’ सुनते। मेरी दोपहरें अकसर सामने के शिव-मन्दिर में बीततीं। वह पुराना मन्दिर शाम और सुबह तो आरती-पूजा के कारण भीड़-भरा रहता व दोपहर को सुनसान। उस समय उसके ठण्डे पत्थर के फर्श पर लेटे रहना मुझे बहुत पसन्द था। छत से बूँद-बूँद जो पानी चूता वह तटहटी तक पहुंचते-पहुंचते गुलाब की खुशबू में बस जाता। उस पानी से मैं गरमी की दोपहर भर मुँह पर छींटे देता रहता।
मेरे पिता पाँच भाई थे। दो वहीं रहते थे। तीन अन्य नगरों में। सभी अपने परिवार सहित ख़ुदागंज में इकट्ठे होते। सोने से लदी, बहुत बूढ़ी दादी अपनी अँधेरी कोठरी में पलंग पर लेटी रहतीं और बारी-बारी से बेटों और बहुओं से खुश या नाराज होती रहतीं। मुझे उस कोठरी में जाने का एक ही लालच था कि वे बड़े घड़े में से निकालकर सोंठ की कतली या मूँग के लड्डू देतीं। पर वैसे वे मुझे बहुत पसन्द नहीं थी।
मुझे अच्छी लगती थी ‘अइया’। वे किसी रिश्तेदार ताऊ की विधवा पत्नी थीं, जिनका गुजर-बसर का कोई दूसरा जरिया नहीं था, अत: वे हमारे परिवार की आश्रिता थीं। तड़के सुबह उठकर आँगन की कुइयाँ से पानी भरना, बरतन माँजना, चौका लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, दादी के पाँव दबाना, सुबह चार बजे से रात दस बजे तक वे मशीन की तरह खटती थीं। सब बहुएँ उनके पाँव तो छूती थीं पर उन्हें नौकरानी की तरह झिड़कती भी थीं।
‘बालसखा’ में परियों की कहानी पढ़-पढ़कर कई बार मैं सोचता कि अइया श्रापग्रस्त रानी है। मैं उनको बहुत चाहता था। उन्हीं के कामकाज में हाथ बँटाता रहता और जब फुरसत मिलती तो उनके साथ छत की दीवार पर बैठकर बातें करता। वे गाँव की नाइनों, धोबिनों, भठियारिनों और डकैतों की घरवालियों के किस्से मुझे सुनातीं और मैं उन्हें अपने भूगोल की कक्षा में पढ़े हुए पाठ-समुद्र क्या होता है, बादल कैसे बनते हैं, यू.पी. में आकर वे कैसे बरसते हैं, हॉलैण्ड के बच्चे काठ के जूते पहनते हैं और एस्किमो बारहसिंगा का दूध पीते हैं-ये कथाएँ सुनाया करता था। मेरी आधी झूठी आधी सच्ची कहानियों की सबसे पहली प्रशंसक अइया थी। एक बार तेज बुखार आया और अइया चल बसीं।
हम लोगों का ख़ुदागंज जाना भी छूट गया। उसका कारण यह था कि मेरे पिता एक प्रकार से अपने परिवार की सामन्ती जमींदारी परम्परा के विद्रोही थे। बाबा और ताऊ चाहते थे कि वे लगान वसूली और लेन-देन का काम सँभाले, लेकिन मेरे पिता छुटपन में ही बरेली चले गये। कुछ पढ़-लिखकर रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में ओवरसीयरी का इम्तहान पास कर आये। बाबा ने मारे गुस्से के बहुत-कुछ सख्त सुस्त कहा तो घर छोड़कर जंगलात के टीले की किसी फर्म में ओवरसीयर होकर बर्मा चले गये और वहाँ सागौन के जंगलों में भटकते रहे। वहाँ से काफी रुपया कमाकर लाये तो मीरजापुर में बसे, वहाँ आटे की चक्की और आटे की मिलें लगायीं पर उनमें नुकसान हुआ और जाने कैसे इलाहाबाद आ बसे। वहाँ अतरसुइया मुहल्ले में मकान बनाया। यह सब मेरे इस संसार में आने के पहले की बातें हैं।
मैंने होश संभाला तो अतरसुइया की गली और माँ-बाप के आर्य-समाजी वातावरण में। माँ कट्टर आर्य-समाजी थीं। मेरे जन्म के पहले मेरे 10 भाई-बहन पैदा होकर मर चुके थे, अत: वे हमेशा मुझे साथ रखतीं। सन्ध्या, हवन, जनेऊ, ब्रह्मचर्य सभी विधिवत्। पिता समझदार आर्य-समाजी थे। वे मुझे हर तरह की किताबें पढ़ने को देते जिनसे माँ परहेज करती थीं। चन्द्रकान्ता सन्तति, भूतनाथ, रक्त मण्डल, चाँद का फाँसी अंक, भारत में अँग्रेजी राज, महात्मा गाँधी की आत्मकथा और चन्द्रशेखर आजाद और भगतसिंह की जीवनियाँ। उस समय का प्रखर तेजस्वी पत्र ‘भविष्य’ हमारे घर नियमित आता था। ख़ुदागंज में कमरबन्द में कटार खोंसकर चलनेवाला बच्चा अब चन्द्रशेखर आजाद की तरह पिस्तौल बाँधकर चलने या ‘रक्त मण्डल’ की तरह अँग्रजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति करने का स्वप्न देखने लगा था।
एक बार ख़ुदागंज से चिट्ठी आयी। ताऊ अशर्फीलाल का देहावसान हो गया था और सबसे छोटे चाचा जमीन-जायदाद का बँटवारा करना चाहते थे। पिता अकेले गये। लौट कर आये तो बहुत थके टूटे-से दिख रहे थे। माँ को उन्होंने जो बताया वह मैंने दरवाजे के पास से सुना। जिन भाइयों को उन्होंने बच्चों की तरह पाला-पोसा और लिखाया-पढ़ाया, नौकरी दिलायी, वे सब इनके खून के प्यासे हो उठे थे। कारण यह था कि जायदाद के हिस्से के अलावा, दादी ने अपने पुराने गहने इन्हें अलग से दे दिये थे। जीवन-भर के विद्रोही बच्चे के प्रति दादी अकस्मात् ममतामयी हो उठी थीं। खूब झगड़े और गाली-गलौज के बाद जीवन-भर ख़ुदागंज न लौटने का प्रण कर वे अन्तिम बार घर को विदा देके चले। बिस्तरा, टीन का ट्रंक और गहने साथ थे। वहाँ से स्टेशन मीरनपुर 12-13 मील दूर है। बैलगाड़ी से जाना होता था। रास्ते में रात हुई और नहर के पासवाले आम के बगीचे में लठैतों ने हमला बोल दिया। ये गहने लेकर एक आम के पेड़ पर चढ़कर छिपकर बैठे रहे। रात-भर लठैत ढूंढ़ते रहे और रात-भर ये छिपे रहे। सुबह होने पर उतरे। असबाब तो लुट चुका था। पोटली लिए स्टेशन पहुंचे। मुँह-हाथ धोकर सन्ध्या की, गायत्री का जाप किया और एक परिचित बूढ़े गाड़ीवाले को गहने की पोटली दी कि दादी को लौटा दे और गहने दूसरे भाइयों की बहुओं को बाँट दिये जाएँ-और चले आये। नमक रोटी कमाएँगे और उसमें खुश रहेंगे।
मैंने उस दिन दरवाजे के पास से यह वृत्तान्त सुना और पिता का भक्त हो गया। उनके मूल्य, उनकी प्रखरता, उनकी उदार दृष्टि, उनकी देश-भक्ति, उनकी समझौता-विहीन ईमानदारी मेरा आदर्श बन गयी...
और फिर आये चरम गरीबी के दिन। पहले पिता ने एक नौकरी स्वीकार की और आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन के नोटिफाइड एरिया के दप्तर में ओवरसीयर हो गये। मेरे बचपन के दो वर्ष मऊनाथ भंजन में बीते। यह सन् 32 का जमाना रहा होगा। उन्हीं दिनों गाँधीजी ने इक्कीस दिन का उपवास किया था। पिता खद्दर और चर्खे के बजाय आजाद और भगतसिंह के प्रशंसक थे, पर उन इक्कीस दिनों में उन्होने एक वक्त खाना नहीं खाया। अन्त में गाँधीजी की पुकार पर सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर इलाहाबाद लौट आये।
और अब शुरू हुए भयंकर गरीबी के दुर्दिन !
पिता कुछ ठेकेदारों वगैरह के लिए नक्शे-वक्शे बनाने का काम करते रहते पर उससे पूरा नहीं पड़ता था। मां के बचे-खुचे गहने वगैरह बेचकर, कुछ कर्ज वगैरह लेकर उन्होंने दो मकान और बनवाये कि ये कुछ काम आएँगे। उसी बीच में माँ सख्त बीमार पड़ गयी और दो साल तक बीमार रहीं। बीमारी की फिक्र और कर्ज की फ्रिक ने पिता को मन और शरीर से तोड़ दिया, पिता सख्त बीमार पड़े और शायद नवम्बर 1939 में उनकी मृत्यु हो गयी। तब मैं 13 वर्ष का था और 8वीं या 9वें दर्जे में था।
उन भयानक दिनों में हमारे दूर के रिश्ते के मामा श्री अभयकृष्ण चौधरी ने बहुत सहायता की। कर्ज उतराने और गुजर-बसर करने के लिए माँ छोटी बहन को लेकर गुरुकुल में नौकरी करने चली गयीं और मैं मामा के पास रहा। मामी ने माँ से बढ़कर स्नेह दिया और मामा ने संरक्षक और अमिट ममता दी, और मैं खूब पढ़ूँ-लिखूँ और कुछ बड़ा काम करूँ-इसकी प्रेरणा वे बराबर मन में भरते रहे। 42 के आन्दोलन में मैंने भाग लिया और सुभाष का बड़ा प्रशंसक बना, और वजीफों तथा मामा की सहायता से पढ़ता रहा। पाठ्य-पुस्तकों के अलावा कविता पुस्तकें तथा अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ने का बेहद शौक रहा और उसी से लेखन के बीज मन में पड़े। उन्हीं दिनों मैंने शेले, कीट्स, वर्डस्वर्थ, टेनीसन, एमिली डिकिन्सन तथा अनेक फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश कवियों को अँग्रेजी अनुवाद में पढ़ा। एमिल ज़ोला, शरतचन्द्र, गोर्की, कुप्रिन, बालज़क, डिकेन्स, विक्टर ह्यूगो, दास्तावस्की तथा तॉल्स्तॉय के उपन्यास पढ़े। तॉल्स्तॉय का ‘वार ऐण्ड पीस’ मेरे जीवन पर स्थायी प्रभाव छोड़ गया।
बी.ए. और एम.ए. की पढ़ाई ट्यूशनों के सहारे चली। कुछ दिन ‘अभ्युदय’ ‘संगम’ और हिन्दुस्तानी एकेडेमी में काम किया। उसी समय ‘मुर्दों का गाँव‘, ‘पृथ्वी और स्वर्ग’ दो कहानी-संग्रह छपे। प्रारम्भिक। उस समय मुझ पर जयशंकर प्रसाद और ऑस्कर वाइल्ड का बहुत प्रभाव था। तभी मैं माखनलाल चतुर्वेदी के सम्पर्क में आया, उन्होंने लिखने को बहुत प्रोत्साहित किया।
एम.ए. कर लेने के बाद मार्क्सवाद का अध्ययन प्रारम्भ किया। प्रगतिशील लेखक संघ का स्थानीय मन्त्री भी रहा कुछ दिन, पर कम्युनिस्टों की कट्टरता तथा देशद्रोही नीतियों से मोहभंग हुआ। तभी मैंने छहों भारतीय दर्शन, वेदान्त तथा विस्तार से वैष्णव और सन्त साहित्य पढ़ा और भारतीय चिन्तन की मानववादी परम्परा मेरे चिन्तन का मूल आधार बन गयी। उन्हीं दिनों पहले ‘गुनाहों का देवता’, फिर ‘प्रगतिवाद एक समीक्षा’ तथा ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा।’ लिखा।
कविता के क्षेत्र में मुझे छायावादी भाषा के बजाय बच्चन, नेपाली, नरेन्द्र शर्मा की काव्यभाषा अधिक ग्राह्य लगी तथा शेले, कीट्स और ऑस्कर वाइल्ड का प्रारम्भिक प्रभाव काव्य-शैली पर रहा। उसी समय ‘अज्ञेय’ से भेंट हुई और ‘अज्ञेय’ ने कुछ कविताएँ ‘दूसरा सप्तक’ के लिए चुनीं। उसके बाद ‘ठण्डा लोहा’ प्रकाशित हुआ।
माँ जरा कट्टर किस्म की आर्य-समाजी थीं। उन्हें यह साहित्यिक लेखन और जीवन बहुत पसन्द नहीं था पर मामा ने बहुत प्रोत्साहन दिया। उस समय तक ‘परिमल’ संस्था काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। मैं उसके प्रारम्भिक सदस्यों में था। मतवाद के घेरे में साहित्य को बाँधना ठीक नहीं है इस बात को लेकर प्रगतिशील लेखकों से काफी विवाद रहता था। तभी नवलेखन के प्रतिनिधि त्रैमासिक के रूप में ‘निकष’ का प्रकाशन शुरू किया। उसी समय ‘नदी प्यासी थी’, ‘चाँद और टूटे हुए लोग’, ‘ठेले पर हिमालय’, ‘सिद्ध साहित्य’ का प्रकाशन हुआ। तब मैं विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगा था। इस दौरान अस्तित्ववादी तथा पश्चिम के अन्य नये दर्शनों का विशिष्ट अध्ययन किया। रिल्के के कविताएँ, कामू के लेख और नाटक, ज्याँ पॉल सार्त्र की रचनाएँ और कार्ल मार्क्स की दार्शनिक रचनाओं में काफी डूबा और साथ ही महाभारत, गीता, विनोबा और लोहिया के साहित्य का विशेष अध्ययन किया। गाँधीजी को भी नये परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की। भारतीय सन्त और सूफी-काव्य विशेषत: कबीर, जायसी और सूर को पुन: पढ़ा और समझा। नाथ परम्परा और सिद्ध साहित्य तो रिसर्च के विषय थे ही।
सन् ’55 के आसपास एक पंजाबी शरणार्थी लड़की से विवाह हुआ। संस्कारों के तीव्र वैषम्य के कारण वह विवाह असफल रहा और बाद में विच्छेद हो गया।
सन् ’60 में बम्बई आ गया। उसके पहले ‘सात गीत वर्ष’, ‘अन्धा युग’, ‘कनुप्रिया’, ‘देशान्तर’ प्रकाशित हो चुके थे। बम्बई आने के बाद ‘बन्द गली का आखिरी मकान’, ‘कहनी अनकहनी’, ‘पश्यन्ती’ प्रकाशित हुए। पुष्पा भारती से विवाह हुआ, जिसने बहुत सुख, सन्तोष और शान्ति दी। केवल जीवन में नहीं वरन् विचारों और साहित्य-चिन्तन के क्षेत्र में भी उनका एक सार्थक गहरा, प्रेरणाप्रद साथ मिला।
इधर पत्रकारिता की व्यस्तता के कारण लिखने का उतना समय नहीं मिल पाता है। कुछ जो लिखा वह छपाया नहीं है।
संक्षेप में जीवन और साहित्यिक प्रगति की यह रूपरेखा है। कैशोर्य तथा ‘परिमल’ युग और बाद में बम्बई जीवन की भी बहुत सी उल्लेखनीय बातें हैं, पर उन सबको लिखूँगा तो पूरी पुस्तक हो जाएगी। अत: इतनी सूचना भेज रहा हूँ जिससे आपका इस समय काम चल जाए।
आपका
सस्नेह,
धर्मवीर भारती
एक ‘अन्तर-व्यू’, एक इण्डरव्यू
(रुद्रनारायण शुक्ल से बातचीत)
न जाने किस भले या बुरे क्षण में यह धारणा मेरे अन्तर में बहुत गहरे पैठकर
स्थापित हो गयी कि लेखक या कवि अगर ‘मनई’ नहीं है तो
उसका
साहित्य-कर्म अच्छा हो या बुरा, ‘मेरे लेखे निरर्थक है। खासी
ऊलजलूल
किस्म की धारणा थी लेकिन उसे धारे रहने का मौलिक अधिकार, किसी भी अन्य
नागरिक की तरह मुझे था, आज है।
प्राय: बीस वर्ष हुए होंगे, लखनऊ में भारती की दो-तीन रचनाएँ पढ़ीं। इन रचनाओं में ताजगी दिखी, स्वच्छता मिली और लेखक में एक आवेग-युक्त आत्मविश्वास का आभास भी हुआ। मन को लगा, कभी इस धर्मवीर भारती नामक व्यक्ति से मिलना चाहिए, कौन जाने ‘मनई’ टाइप का आदमी है। कुछ दिनों बाद, इलाहाबाद जाना हुआ। उन दिनों ‘संगम’ साप्ताहिक का प्रकाशन आरम्भ हो चुका था। भारती उसमें संयुक्त सम्पादक थे। मैं सम्पादकी का पेशा छोड़, उत्तर प्रदेश में ‘ब्लिट्ज’ के विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। ‘निराला’ जी इलाहाबाद में ही थे। बहरहाल, प्रयाग की उस यात्रा का वह दिन आज भी याद आता है। सुबह से तीसरे पहर तक निरालाजी के साथ बीता, पंजा लड़ाते, ऊंचाई नापते, खैनी-तमाखू चबाते और उपलों की आँच पर खीर पकाते, और निरालाजी की हिन्दी-अँग्रेज़ी सूक्तियाँ और कटूक्तियाँ सुनते। मैंने भारती का नाम लिया तो बोले ‘‘आइ थिंक ही राइट्स वैल, ही हैज नॉट कम्पैल्ड मी टु रीड हिज वर्क्स, आइ ऐम नॉट इण्टिमेट मच, व्हाइ नॉट यू सी हिम..देखो शायद दमदार हो। हू नोज़ !’’
सन् 1949 का प्रयाग में वह दिन और वह शाम आज तक याद है। शाम को दारागंज से अपने ठीहे पर, बार्नेट होटल लौटा और उसी शाम-रात भारती से भेंट हुई। मेरे दो बुजुर्ग दोस्त श्री भगवतीचरण वर्मा और श्री वाचस्पति पाठक साथ थे। घण्टे-डेढ़ घण्टे गपशप रही, और ऐसा लगा कि एक कतरे से कहीं ज्यादा खून इस धर्मवीर भारती नामक व्यक्ति से दिल-दिमाग को भिगोता रहता है। दूसरी चीज उस पहली मुलाकात की जो याद है वह है भारती का अट्टहास। मुक्त कण्ठ से हँस पड़नेवाले हर नर-नारी के प्रति मेरे मन में एक प्रशंसा का भाव सदा से रहा है; और प्रेमचन्दजी, स्व. बैरिस्टर छेदीलाल और फिर श्रीपत राय और अमृत राय के प्रति मेरे मन में स्नेह और आदर जगाने के कारणों में इन सबकी ठहाका-क्षमता का कुछ–न-कुछ हाथ रहा है। भारती का अट्टाहस और बेसाख्ता हंस पड़ने की आदत, मुझे ठीक याद है, उस रात मुझे खूब अच्छी लगी थी।
प्राय: बीस वर्ष हुए होंगे, लखनऊ में भारती की दो-तीन रचनाएँ पढ़ीं। इन रचनाओं में ताजगी दिखी, स्वच्छता मिली और लेखक में एक आवेग-युक्त आत्मविश्वास का आभास भी हुआ। मन को लगा, कभी इस धर्मवीर भारती नामक व्यक्ति से मिलना चाहिए, कौन जाने ‘मनई’ टाइप का आदमी है। कुछ दिनों बाद, इलाहाबाद जाना हुआ। उन दिनों ‘संगम’ साप्ताहिक का प्रकाशन आरम्भ हो चुका था। भारती उसमें संयुक्त सम्पादक थे। मैं सम्पादकी का पेशा छोड़, उत्तर प्रदेश में ‘ब्लिट्ज’ के विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। ‘निराला’ जी इलाहाबाद में ही थे। बहरहाल, प्रयाग की उस यात्रा का वह दिन आज भी याद आता है। सुबह से तीसरे पहर तक निरालाजी के साथ बीता, पंजा लड़ाते, ऊंचाई नापते, खैनी-तमाखू चबाते और उपलों की आँच पर खीर पकाते, और निरालाजी की हिन्दी-अँग्रेज़ी सूक्तियाँ और कटूक्तियाँ सुनते। मैंने भारती का नाम लिया तो बोले ‘‘आइ थिंक ही राइट्स वैल, ही हैज नॉट कम्पैल्ड मी टु रीड हिज वर्क्स, आइ ऐम नॉट इण्टिमेट मच, व्हाइ नॉट यू सी हिम..देखो शायद दमदार हो। हू नोज़ !’’
सन् 1949 का प्रयाग में वह दिन और वह शाम आज तक याद है। शाम को दारागंज से अपने ठीहे पर, बार्नेट होटल लौटा और उसी शाम-रात भारती से भेंट हुई। मेरे दो बुजुर्ग दोस्त श्री भगवतीचरण वर्मा और श्री वाचस्पति पाठक साथ थे। घण्टे-डेढ़ घण्टे गपशप रही, और ऐसा लगा कि एक कतरे से कहीं ज्यादा खून इस धर्मवीर भारती नामक व्यक्ति से दिल-दिमाग को भिगोता रहता है। दूसरी चीज उस पहली मुलाकात की जो याद है वह है भारती का अट्टहास। मुक्त कण्ठ से हँस पड़नेवाले हर नर-नारी के प्रति मेरे मन में एक प्रशंसा का भाव सदा से रहा है; और प्रेमचन्दजी, स्व. बैरिस्टर छेदीलाल और फिर श्रीपत राय और अमृत राय के प्रति मेरे मन में स्नेह और आदर जगाने के कारणों में इन सबकी ठहाका-क्षमता का कुछ–न-कुछ हाथ रहा है। भारती का अट्टाहस और बेसाख्ता हंस पड़ने की आदत, मुझे ठीक याद है, उस रात मुझे खूब अच्छी लगी थी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i