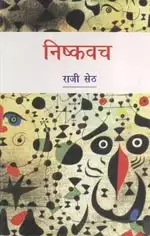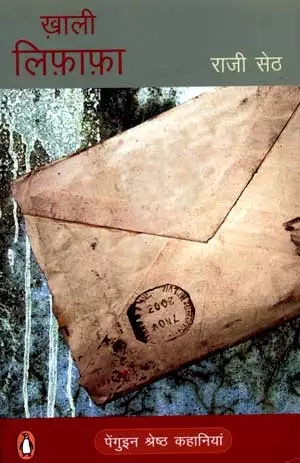|
सामाजिक >> निष्कवच निष्कवचराजी सेठ
|
100 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है मार्मिक उपन्यास...
Nishkavach
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
पिछले दो दशकों में हिन्दी कथा-लेखन के क्षेत्र में अपनी महत्त्वपूर्ण पहचान बनाने वाली लेखिकाओं में अग्रणी राजी सेठ की नवीनतम औपन्यासिक कृति है ‘निष्कवच’।
‘निष्कवच’ में मूल्यों की डगमगाहट में अपने मूल से उखड़ी युवा पीढ़ी की मानसिकता में से उभरते दो वृत्तान्त हैं। यह दो अलग-अलग कथाएँ हैं, पर नहीं भी हैं दोनों वृत्तान्तों में केन्द्रीय पात्रों के निष्कवच यथार्थ के सामने पटक दिये जाने का एक साझा कालगत और परिवेशगत रिश्ता है। यहाँ इनके अपने दर्द हैं, अपने तर्क, जिन्दगी से निपटने के अपने आवेश निर्देश हैं।
कहना न होगा कि इनमें जो असुरक्षा और बेचैनी है वह अब तक अनदेखी रहती आयी है, क्योंकि हमारी सोच वयस्क पीढ़ी की संवेदना पर झुकी हुई है। दरअसल उनकी बेखबर करवटों-तले बहुत से नाजुक आवेग पिसते आये हैं।
‘निष्कवच’ के दोनों वृत्तान्तों के पात्रों का ऐसा जूझना कहीं-न-कहीं मूल्यों के संक्रमण की गवाही भी देता है। जिन मान्यताओं से अब तक काम चलता रहा है, अब नहीं चल रहा। एक स्निग्ध सुरक्षित संसार की तलाश पिछले मूल्यों को ध्वस्त जरूर करती है, पर एक नया जुझारु साहस जुटाने के लिए सम्बद्ध भी होती है। जाहिर है, परिवेश में पनप रहे इन संघर्षों का समाज को तो अभ्यस्त होना है।......
राजी सेठ की यह नवीनतम कथाकृति अपने पूरे वैचारिक साहस के साथ जीवन और परिवेश के यथार्थ की एक सशक्त एवं सार्थक अभिव्यक्ति है।
‘निष्कवच’ में मूल्यों की डगमगाहट में अपने मूल से उखड़ी युवा पीढ़ी की मानसिकता में से उभरते दो वृत्तान्त हैं। यह दो अलग-अलग कथाएँ हैं, पर नहीं भी हैं दोनों वृत्तान्तों में केन्द्रीय पात्रों के निष्कवच यथार्थ के सामने पटक दिये जाने का एक साझा कालगत और परिवेशगत रिश्ता है। यहाँ इनके अपने दर्द हैं, अपने तर्क, जिन्दगी से निपटने के अपने आवेश निर्देश हैं।
कहना न होगा कि इनमें जो असुरक्षा और बेचैनी है वह अब तक अनदेखी रहती आयी है, क्योंकि हमारी सोच वयस्क पीढ़ी की संवेदना पर झुकी हुई है। दरअसल उनकी बेखबर करवटों-तले बहुत से नाजुक आवेग पिसते आये हैं।
‘निष्कवच’ के दोनों वृत्तान्तों के पात्रों का ऐसा जूझना कहीं-न-कहीं मूल्यों के संक्रमण की गवाही भी देता है। जिन मान्यताओं से अब तक काम चलता रहा है, अब नहीं चल रहा। एक स्निग्ध सुरक्षित संसार की तलाश पिछले मूल्यों को ध्वस्त जरूर करती है, पर एक नया जुझारु साहस जुटाने के लिए सम्बद्ध भी होती है। जाहिर है, परिवेश में पनप रहे इन संघर्षों का समाज को तो अभ्यस्त होना है।......
राजी सेठ की यह नवीनतम कथाकृति अपने पूरे वैचारिक साहस के साथ जीवन और परिवेश के यथार्थ की एक सशक्त एवं सार्थक अभिव्यक्ति है।
वृतांत एक
मेरे लिए सब कुछ वहीं का वहीं खड़ा है।
इस टेबल से लगी खिड़की के पार का दृश्य वैसा है का वैसा है। दीठ के विस्तार को बीच में कहीं से टोक देती शिवमन्दिर की गुम्बद और धूप के क्रोध से अवर्ण हो गयी उस पर फहराती पताका। मन्दिर की आड़ में वही बँगले। उन पर कुछ और आवेश में झूलती लतरें और बीच में काले अजगर-सी लेटी लम्बी सड़क। आगे चलकर दायें को एकदम नदी का रेतीला पाट आ जाता है इसलिए मैदान की मिट्टी भी चमकती चिलमिलाती रहती है।
सब कुछ वही है। वैसा का वैसा। किसी चौखटे में बँधे चित्र की तरह। एक मैं ही यहाँ नहीं था। कॉलेज हॉस्टल के गलियारों से चलता-चलता प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन सबके बीच आन बैठा हूँ।
फिर उसी तरह बैठा हूँ। पहली मंजिल पर उसी खिड़की से लगकर। उसी टेबल पर। उसी लैम्प के प्रकाशवृत्त के नीचे। लगता है काठ की कुरसी पर सीधा बैठा ऊँघता-जागता, पढ़ता-लिखता मैं वहीं चिपका रह गया हूँ।
पर वह ? उसके लिए जीवन कैसे दौड़ता-फलाँगता तीन-तीन मंजिलें पार करता गया है। मेरे देखते-ही-देखते वह बच्ची माँ बन गई और एक उगते हुए जीवन का संचालन उसके हाथ में आ गया है। उसे कैसा लग रहा होगा ? कल्पना करता हूँ। नहीं फलती। मातृत्व के साथ जैसे बड़प्न की गन्ध है वह छवि के साथ नहीं चिपकती। इस सारे होने में क्या उसकी भी इच्छा शामिल होगी यों ही बस।.... शायद उसका बस चला होता तो वह अपने को इस दायित्व के हवाले कभी न करती।
रमण के संसर्ग में धधकते अपने पूरेपन की आभा को लम्बाये रखती। डेढ़ साल। होता ही कितना है डेढ़ साल ! उसमें से भी नौ महीने.....
‘‘एक पत्र तुम भी उसे लिख देना, ’’ कहती हुई मां अलमारी में से अपने कपड़े़ लेकर बाहर चली गयी हैं और मुझे एक और खूँटे से बाँध गयी हैं।
कागज लेकर बैठता हूँ पर हाथ ही नहीं चलते। क्या लिखना ठीक होगा। यह कि मैं खुश हो रहा हूँ या मुझे बहुत ही अटपटा लग रहा है या कि हम सब, मेरा मतलब है माँ पापा बहुत ही खुश हैं। नहीं, नहीं, यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि अब तो तुम सच में बड़ी हो गयी हो। तुम्हें बधाई देता हूँ। मन से।
शब्द खोखले लगते हैं। बजते हुए ! उछाह और प्रवाह के बिना। यहाँ से कुछ चलेगा ही नहीं तो पहुँचेगा कैसे ! यह व्यायाम व्यर्थ होगा। उसे आशा ही कहाँ होगी कि मेरा पत्र आएगा ! वह देना पाना हमारे बीच बना ही कब था ! उस पारस्परिकता ने जन्म ही कहाँ लिया जबकि उस काल में वही सबसे स्वाभाविक बात रही होती। कहने को हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे, एक ही दरवाजे से घुसते-निकलते थे। एक ही दिनचर्या के अधीन रखे जाते थे। पर.....
एक तटस्थ-सा भाव उसके लिए मेरे मन में क्यों रहा,. इसे मैं आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। मौसी यानी माँ की चचेरी बहन की लड़की की तरह उसने इस घर में अचानक प्रवेश पाया था। मैं तब सातवें या शायद आठवें में था।
अपने उस एकान्त में एक साथी पा जाने की मुझे कोई खाश खुशी नहीं हुई थी। न नकार। शायद तब तक मेरे आसपास सबकुछ तय हो चुका था। मेरे खेल और मेरी रुचियाँ अपनी परिधि टटोलकर अपने मनचीते केन्द्रों में स्थिति हो चुकी थीं। रुचियों का पुल उसके मेरे बीच नहीं बन पाया था।
उसकी खाट मेरे कमरे में बिछा दी गयी थी। वह मेरे साथ स्कूल जाने लगी थी। मेरे साथ खाना खाने लग गई थी। पता नहीं कहाँ से पा गये उत्साह से माँ मुझे उधर ठेलने लगी थी। मेरे लिए उस साहचर्य की जरूरत और सघनता को माँ ने स्वयं तय कर लिया था। उतनी ही ललक और उत्साह से मैं प्रस्तुत न हो पाऊँ तो माँ कुपित होने लग गयी थी वह क्यों मेरे साथ बैडमिण्टन खेलने नहीं जा रही थी। उसे तैरने ले जाने में मुझे क्या तकलीफ है जबकि पापा ने क्लब के कार्ड में उसका नाम बढ़वा लिया है....मैं क्यों उसकी रुचियों और रुझानों के विकास पर कोई ध्यान नहीं देता। जबकि मैं उससे बड़ा हूँ..,...।
याद करूँ तो मेरे आसपास जो संसार था, उसमें इस अचानक के प्रवेश का कोई स्थान नहीं था। कुछ भी मेरे मन में साफ नहीं था। न उस पर अपने अधिकार के बारे में, न उसके प्रति अपने कर्तव्य को लेकर। माँ मुझे टोकतीं। ताड़ना देतीं। वंचित करतीं। अपना पुत्र होने की अतिरिक्तता को मुझसे छीन-झपट कर उसके हवाले कर देना चाहतीं। याद नहीं पड़ता- माँ ने उसे कभी खास डाँटा-फटकारा हो। मुझे तो ठीक से यह भी अनुमान नहीं था कि माँ की डाँट-फटकार के प्रति उसकी सहिष्णुता थी कितनी !
आज सोचता हूँ, माँ क्यों करती थी ऐसा। बड़ी–छोटी उँगली को खींच-खाँच कर बराबर कर देना चाहती थीं। ऐसा होता है क्या ? हो सकता है क्या ? वह भी एकाएक बीच में। बिना किसी स्पष्ट कारण या तैयारी के।
आत्मगरिमा को पाने का, या अपनी ही न्यायप्रियता पर रीझने का माँ के पास शायद यही एक ढंग होगा। लगता होगा कैसे हँसते-हँसते वह किसी पराये को श्रेय दे देती हैं। अपने पर कठोर हो लेती हैं। ऐसा कितने लोग कर पाते हैं, करने की चेष्टा में फूहड़ हो जाते है, क्योंकि नैसर्गिक सम्बन्ध तो चुप रह सकता है, शिराओं में बजता है। ओढे़ हुए सम्बन्धों को जताना-प्रकटाना पड़ता है।
इन सब बातों ने भी उसके प्रति मेरी तटस्थता को धारदार ही बनाया होगा। माँ के दिए ममत्व को वह प्रकट प्रीति से भोगती थी। किशोरी से बच्ची बनने की कृत्रिमता को ओढ़ती थी। इतराती थी और ध्यान खींचते-खींचते केन्द में सरकती चली आती थी जबकि मुझे ‘अपनी उम्र से बड़ा’ कहकर अपने पैरों के नीचे की जमीन से बेदखल कर दिया जाता। ऐसा करते समय भी असल में वे ऐसे परिपक्क बच्चे के जन्मदाता होने के उपलक्ष्य में अपना ही अभिषेक कर रहे होते । मैं एक उदाहरण ! मैं एक अनूठा ! ‘‘भई, बड़ा ही धीरज है, कभी इस लड़के में न कोई अनुचित हठ...न शरारत !’’ अब लगता है, कभी हठ या शरारत की होती तो उन्हें आघात ही लगता।
इन बातों का कुछ खास बोझ पड़ता रहा हो, याद नहीं पड़ता। मुझे भी शायद यही अनुकूल पड़ता रहा होगा। दोस्तों के लम्बे झुण्ड मुझे उबाते हैं। यह ऊब निश्चय ही दोस्तों को भी मुझसे होती होगी, नहीं तो ‘चूजी’ कह-कहकर हर समय वे मेरा बहिष्कार करने की ताक में न रहते। इलाहाबाद में भास्कर और दिल्ली में बासू के सिवा अभी तक मेरा कोई अंतरंग दोस्त नहीं है। अकेलापन मुझे उबाता नहीं, बल्कि बहुत दिनों तक उपलब्ध न हो तो क्षुब्ध करता है।
उसके आने के बाद भी मुझे अकेला ही कहा जाए तो ठीक ही होगा। इस स्थिति का कष्ट न उसके आने के पहले था, न बाद में था। कष्ट कुछ था तो माँ के हाथ में पकड़ी लोहे की मापक छड़ का, जो हर चीज को एक ही सीध में मापना चाहती थी। अब वह इस घर में नहीं रहती। अपना कहे जाने वाले घर में रहती है।
एम.ए. और उसके बाद एल.एल.बी करके जब वह घर लौटा था तो वह मुझे एकाएक बड़ी जैसी लगी थी। गठन, उठान, उग्रता। माँ ने कहा था लड़कियाँ जल्दी सयानी हो जाती हैं- ब्याहने योग्य। उत्सुकता में मैंने उससे एक दिन पूछा था- ‘‘तुम्हें ठीक लगता है क्या इतनी जल्दी शादी-वादी का किस्सा ?’’ चूंकि मेरे लिए यह बात अकल्पनीय थी। कोई भी हम उम्र संगी-साथी, परिचित इस तैराकी के लिए तैयार नहीं था। प्राथमिक थी दिशा की तलाश। कैसे कोई बिना
सोचे ऐसे सागर में कूद जाए, जहाँ से कभी वापसी भी सम्भव नहीं।
मेरे प्रश्न से वह टँग-सी गयी- ‘‘कभी तो लगता है फालतू में बँध जाएँगे ! फिर लगता है बड़ा अच्छा लगेगा। कोई बिल्कुल अपना तो होगा।’’
मैं जैसे सन्नाटे में। वह हम लोगों को गाली दे रही थी। विशेष तो माँ को, जो उसको माँ देने के उत्साह में अपनी देह के रोएँ भी फूँक रही थी। मेरी प्रतिक्रिया पर उसका ध्यान नहीं था। वह अपनी रौ में थी।
‘‘कितना अजीब होता है न इतनी बड़ी दुनिया में कुछ भी अपना होना....कितना हताश करता है....’’ उदासी का एक चिथड़ा उसके उजले गालों को फटकारता निकल गया। मेरे सामने बैठी इस समय वह मुझे ऐसी लगी थी जैसी कभी लगती नहीं थी-अन्तरंग, आर्द्र, उदास।
‘‘क्यों मौसी तो हैं न, वह...’’
‘‘ऊँह !’’ उसने मुझे अधबीच टोक दिया था, ‘‘तुम मेरी मम्मी की बात कर रहे हो न ? मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके लिए। जब जहाँ चाहा, ठेल दिया। मेरी पढ़ाई-लिखाई की बात को प्रमुख बनाकर....’’
‘‘तुम गलत कहती हो ! सुना तो यह है कि तुम्हारे कारण उन्होंने अपना दुःख-सुख नहीं देखा। जबकि चाहतीं तो फिर अपना घर बसा सकती थीं।’’
‘‘उसमें अभी क्या कमी है। स्कूल की वह छोटी-छोटी छोकरियाँ उन्हें ज्यादा प्यारी लगती हैं, क्योंकि हर समय आसपास मँडराती रहती हैं। यह मुझसे नहीं होता। तुम्हें नहीं पता बड़ी काइयाँ हैं ये लड़कियाँ खूब फुलाना-फुसलाना जानती हैं। दे नो हाउ टु फीड हर ईगो। टु गेट द बेस्ट आउट ऑफ हर। ...और मम्मी भी उनकी बातों में आ जाती हैं। तुम्हें एक बात बताऊँ....’’
वह पलँग के परले सिरे से सरककर मेरे निकट आ गयी थी, जैसे कोई बड़े भेद की बात कहने जा रही हो-‘‘सच तो यह है कि वह मुझे कभी अपनी माँ ही नहीं लगतीं। कुछ कहते रहो, कभी नहीं समझतीं ! बस, हर समय पट्टी-स्लेट लेकर बैठे रहो छोकरियों से बतियाते रहो। मन से उनसे मेरी एक मिनट को नहीं बनती। काश ! मेरी भी तुम्हारे जैसी माँ होती....’’
‘‘है तो सही। वह तुम्हारी भी तो माँ हैं।’’ –मैं द्रवित हो गया था।
‘‘नहीं ! वह तुम्हारी माँ हैं, मेरी माँ नहीं। आण्टी तो आण्टी ही होती हैं। ’’
गड्ड-मड्ड-सा उसका चेहरा एकाएक मुझे पिघला-सा लगा था। मैं अस्थिर हो गया था। अभी एक तो मैं अपनी ही दुखती रगों को जानता था।
क्या विडम्बना थी, उसके कारण मेरी माँ भी छिनती है और मेरी माँ उसे अपनी माँ भी नहीं लगती...पर उस समय तो मैं उसकी संजीदगी से ही आन्दोलित था। पता ही नहीं वह कैसे भूली-सी उस कगार पर आने लगी थी। वैसी अपनापे-भरी बात उसने मुझसे पहली बार कही थी-अन्तरंग तरीके से। ज्यादातर वह असहज और प्रतिक्रिया प्रधान मुद्रा में रहती है। रिश्तों के प्रति अनादर से भरी।
मैं सोच में पड़ गया था। क्षणिक ही सही, पर क्या चीज थी जो उसे इस अन्तरंगता के क्षण तक ला सकी थी। इस पुल को न बनने देने में क्या कहीं मैं भी दोषी था ?
ससुराल चली जरूर गयी थी फिर भी जैसे इसी घर में थी। कभी इस कारण तो कभी उस करण से माँ की चिन्ताओं के घेरे में। जाने किस सजातीय साँकल से बँधी। जिन दिनों मैं एम.ए. के लिए इलाहाबाद चला गया था, उन दिनों उसका रिश्ता माँ से गहरा हुआ होगा। मैं वैसे भी सदा हाशिये पर ही बना रहता था। एक तो मैं उद्घोषित चुप्पा ! फिर एक के बाद दूसरी परीक्षाओं का भार ! कुछ अपनी ही स्थिति और स्वप्र के बीच के तनाव। मैं जैसे घर में होता ही नहीं था।
‘‘अच्छा, तुम बताओ, जाना चाहिए न ? अभी तो उसकी डिलीवरी से निपटकर आयी हूँ ! ’’माँ ने कमरे में घुसते ही अपनी दुविधा पसार दी।
‘‘पर कहाँ ?’’
‘‘अरे, ऑपरेशन हुआ है न उसका। रमण की चिट्ठी आयी है।’’
‘‘कैसा ऑपरेशन.....किसका ऑपरेशन....?’’
माँ को अपनी भूल पता लगती है। बात के सभी छोर अभी तो उसकी मुट्ठी में ही हैं। ‘‘अब तुम्हें क्या बताऊँ, उसकी छाती में.....मेरा मतलब है उसके ब्रेस्ट में गिल्टी प़ड़ गयी थी। मवाद भर गया था। काफी गहरा काटना पड़ा !’’
‘‘कैन्सर है क्या ?’’ मैं काँप जाता हूँ।
‘‘ऊह ! कैन्सर कहाँ से हो जाता है अकसर ऐसा, बच्चे को दूध नहीं पिलाया होगा। अब तू....’’
माँ संकोच में हैं। इतना भी वह पता नहीं कैसे बोल गयीं। शायद चिन्ता का तार उसके मन में अभी टूटा नहीं है। पापा के कहने पर यह बात स्पष्ट हो गयी है।
‘‘यह अब नया चला है, ’’ पापा का नाश्ता रखते माँ बोलती जाती हैं। ‘‘तुम्हें मालूम है, ऐसा क्यों हुआ....बच्चों को दूध पिलाने से इनकी फिगर बिगड़ती है न....।’’
मेरे कान खड़े हो जाते हैं। ‘‘अब जैसे नहीं बिगड़ेगी इस काटपीट से। फैशन के मारे मरी जाती हैं ये लड़कियाँ !’’
कुछ-कुछ साफ होने लगता है मन में। कड़ियाँ जुड़ती हैं। वह ऐसी ही मिट्टी की बनी हैं। उमगायी ललसायी हुई। जीवन को चाँपकर रखने के चाव से भरी हुई। अपनी जरूरतों के प्रति एकदम चटक चौकन्नी। माँ को यह ललक डराती थी। उसकी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में की आत्मनिर्भरता को जरूरी समझते हुए भी उसके हाथ पीले कर देना चाहती थी।
पढ़ने जैसा पराक्रम का उसे शौक नहीं था, और मैं था कि एक तरह की पुस्तकों से ऊबने पर दूसरी तरह की पुस्तकों में डूबता था। केवल सन्दर्भ और विषय बदल जाते। थुल-थुल रेत में खड़ी पाठ्यक्रम की नाव मेरे लिए सदा विविध प्रसंगों वाली नदी में खुलती।
वह अकसर आँगन में तसला रखकर पैर भिगोये बैठी रहती। फिर उन्हें पोंछती। फिर क्रीम लगाती। मुँह रगड़ती। कपड़े सभाँलती। बार-बार शीशा देखती। पलंग पर पसरकर छत देखती रहती। मेरी तरह नहीं कि एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक से तीसरी ! तीसरी से डायरी। फिर किताब, फिर कॉपी, फिर ‘पजल’ फिर स्टीरियो। मक्खी की तरह मुझे इधर से उधर कूदते देख वह मेरी खिल्ली-सी उड़ाती। होठों में बन्द एक तरेर जैसी उसके चेहरे पर छाप जाती। पलँग पर पैर लटका कर अपनी ठुड्ढी के नीचे दोनों हाथ टेककर वह अपनी आँखों को जिधर जिधर मैं जाता, उधर घुमाती रहती।.... ऐसा आमोद से भरा फुर्सती-सा उसका अन्दाज !
अकसर किसी कॉमिक्स या किताब को बेध्यान-सा होकर उठाती और पढ़ने लगती। पूरा डूब जाती, पर यह डूबना उसमें और अधिक डूबने का उत्साह पैदा कर दे, ऐसा बन नहीं पाता था। पुस्तक को ऐसे निवृत्त भाव से किनारे रखती जैसे किसी अटपटे काम को कर लेने के बाद आराम जरूरी हो।
क्यों उसमें वह बेचैनी पैदा नहीं होती थी, जो उसके समवयस्कों को हर समय पंजे पर खड़ा रख सकती थी।
वह अपने को खाली और खुला छोडे़ रखती, ऐसे जैसे कहीं कुछ होने को है कोई अचम्भा जैसा घट जाने को है। यह व्याख्या भी मुझे आज सूझ रही है। तब तो उसे यूँ पड़े-पड़े छत ताकने या पैर हिलाते देख खीझ चढ़ जाती थी।
‘‘इतनी किताबें लाकर देता हूँ लायब्रेरी से पढ़ती क्यों नहीं ?’’
ऐसे जवाब-तलब का उसने अकम्प उत्तर दिया था-‘‘नहीं पढ़ती तुम्हें क्या नम्बर तो कम नहीं आते !’’
‘‘नम्बर तो सबक घोंट कर भी आ जाते हैं, पर इससे ज्यादा क्या कुछ जानना नहीं होता ?’’
उसका चेहरा वैसा ही- उद्धत, आत्मतृप्त। भर्त्सना की नोक को मेरी ओर घुमाता हुआ- ‘‘अच्छा बस ! तुम्हें किताबें चाटनी हैं तो चाटो। मैं तो अभी बासू आएगा तो उसके साथ बैठकर शतरंज खेलूँगी।
उफ्फ ! बासू...बासू !.....बासू ! मेरे लिए भी तो वही एक था। वही एक अकेला।
परिचितों की भीड़ को काटता, किसी सुभग घड़ी वह मुझ तक चलता चला आया था और मेरी बगल में खड़ा हो गया था। इस तलाश का श्रेय भी उसे ही था। मेरे लिए तो वह ‘यह नहीं’, ‘यह भी नहीं’ के दम्भी नकार को चकनाचूर कर देने वाला एक अनूठा चमत्कार था।
वह था तो बस था, जैसे हजारों विखण्डित चीजें इस ब्रह्माण्ड में घूमती हैं और अपने पूरेपन को पा लेने के लिए किसी परिचित परिक्रमा-पथ में घुस लेती हैं। हार्दिकता के सत्त्व को उकेर लेती हैं।
मैं खिंचता आया था या बासू, नहीं जानता। मित्र पा जाए, ऐसा आन्तरिक संकट उसके जैसे व्यक्ति को क्योंकर रहा होगा। वह तो अकेला रह सकता था। रह तो मैं सकता था पर उसके और मेरे अकेलेपन में फर्क था अनवरत अशान्त था। वह आत्म-सम्पन्न। मैं एक से दूसरी से तीसरी व्यस्तता में अपने को बींध कर पहले ही प्रतिबन्धित और सुरक्षित कर लेता था। वह बेपरवाह था-फक्कड़ और मुक्त। जहाँ बैठ गया वहीं पर पूरा। वह सब कहीं जम सकता था। उसका सब कहीं प्रवेश था- हर किस्म की टोली में। बलियाटिक्स और बीटल्स, हिप्पी और हारे, अगुए और पिछलगुए- सबके साथ। सबमें रहते हुए भी वह अपने स्वत्व को अछूता रख लेता था। कोई कच्चापन कहीं दीखता तभी न कोई उसे छोड़ता। उसके मन तक पहुंचने के लिए उसकी निहायत उत्कट और उदग्र दृष्टि के सामने से गुजरना पड़ता था। वह सामना किसी भी प्रकार के आश्वासन से खाली होता था, रूखा-सूखा, असान्त्वनीय। जो कोई इस खुरदरेपन को झेल सकता होगा, वही तो उसकी आन्तरिकता तक पहुँचेगा।
मैं जाने क्यों, उसी को लेकर बहक रहा हूँ। क्या वह मेरे भीतर इतना खुला हुआ, इतना विद्यमान है कि अपनी अनुपस्थिति को भी अपनी मनोमयता में तब्दील कर दे सकता है। उन दिनों के बाद मुझे उसका कोई अता-पता नहीं। पूरे दो वर्ष....।
पिछले सप्ताह ‘एक्सप्रेस’ के तीसरे पन्ने पर उसकी फोटो देखी थी। दिल्ली कन्याकुमारी तक जाने वाली टोली के अगुआ के रूप में। अचम्भा नहीं हुआ था। यह दल उसी ने तैयार किया होगा। इतनी उर्जा उसके भीतर है। बल्कि इसलिए इतनी आतंककारी उदग्रता उसमें है। उसे ऐसा कुछ करते देखकर लगता है कि ऊर्जा के इस अक्षय आवेग में खपत हो जाना अच्छा है। यह उसके हित में है। उसके सामान्य हो सकने के लिए जरूरी है।
चाहे यह बहस उसकी सदा-सदा जारी रहा करती थी कि हम सब क्यों सदा साधारण-सामान्य के हक में बने रहते हैं। हर नये संयोजन के विरुद्ध अडे़ रहते हैं। यह काम फिर जबरजस्ती कोई साधारण व्यक्ति या परिस्थिति हमसे करवाती है।
‘‘तुम्हें मालूम है विशाल, हम ऐसा क्यों करते हैं ? असाधरणता हमें हमेशा आतंकित करती है क्योंकि तुलना में अपने को हलका और पुराना सिद्ध करके फेंक देती है।’’
आश्चर्य जरूर है कि मैं उसके साथ ऐसी किसी आतंककारी अनुभूति से क्यों कर बच गया था। मिलते ही मुझे लगा था कि वह मेरे ही अस्तित्व का एक जरूरी हिस्सा है, जिसे सामने रखकर मैं अपनी अब तक की तलब और तड़प के स्वभाव को जान पा सकता हूँ। बिना यत्न के स्वत्व तक पहुंच और पहुँचा रहा हूँ। उससे वह बातें होती थीं, सदियों से भीतर तन्द्रिल पड़ी हैं ...पात्र को पाकर जागेंगी नहीं तो अव्यक्त रह जाएँगी, क्योंकि उन कोषों का कोई सिद्ध व्यावहारिक पक्ष तो नहीं होता।
आश्चर्य यह भी है कि हम दोनों एकदम अलग-अलग मिट्टी के बने थे। मैं यदि दुबला, कुछ-कुछ नाजुक, चिड़चिड़ा, अतिरिक्त संवेदनशील, अन्तर्मुखी और भावुक हूँ तो वह पुरुषों का भी पुरुष, मांसल, युक्त और आत्माश्वस्त। एकदम विपरीत। हमारा सम्बन्ध ऐसा, जैसे दो बाँसों के बीच बँधी रस्सी का साफ-सुथरा तनाव। एक-दूसरे का अकृत्रिम स्वीकार।
जोखिम की हदों से टकराता साहस उसमें कहाँ से आता है, मैं जल्दी नहीं समझ सका। कभी माँ-बाप के प्रसंग के माध्यम से उसकी जड़े़ टटोलने की कोशिश की तो उसने झटक दिया-बेरहमी से। यह जताते हुए कि वहाँ जाना बेकार है।
इस टेबल से लगी खिड़की के पार का दृश्य वैसा है का वैसा है। दीठ के विस्तार को बीच में कहीं से टोक देती शिवमन्दिर की गुम्बद और धूप के क्रोध से अवर्ण हो गयी उस पर फहराती पताका। मन्दिर की आड़ में वही बँगले। उन पर कुछ और आवेश में झूलती लतरें और बीच में काले अजगर-सी लेटी लम्बी सड़क। आगे चलकर दायें को एकदम नदी का रेतीला पाट आ जाता है इसलिए मैदान की मिट्टी भी चमकती चिलमिलाती रहती है।
सब कुछ वही है। वैसा का वैसा। किसी चौखटे में बँधे चित्र की तरह। एक मैं ही यहाँ नहीं था। कॉलेज हॉस्टल के गलियारों से चलता-चलता प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन सबके बीच आन बैठा हूँ।
फिर उसी तरह बैठा हूँ। पहली मंजिल पर उसी खिड़की से लगकर। उसी टेबल पर। उसी लैम्प के प्रकाशवृत्त के नीचे। लगता है काठ की कुरसी पर सीधा बैठा ऊँघता-जागता, पढ़ता-लिखता मैं वहीं चिपका रह गया हूँ।
पर वह ? उसके लिए जीवन कैसे दौड़ता-फलाँगता तीन-तीन मंजिलें पार करता गया है। मेरे देखते-ही-देखते वह बच्ची माँ बन गई और एक उगते हुए जीवन का संचालन उसके हाथ में आ गया है। उसे कैसा लग रहा होगा ? कल्पना करता हूँ। नहीं फलती। मातृत्व के साथ जैसे बड़प्न की गन्ध है वह छवि के साथ नहीं चिपकती। इस सारे होने में क्या उसकी भी इच्छा शामिल होगी यों ही बस।.... शायद उसका बस चला होता तो वह अपने को इस दायित्व के हवाले कभी न करती।
रमण के संसर्ग में धधकते अपने पूरेपन की आभा को लम्बाये रखती। डेढ़ साल। होता ही कितना है डेढ़ साल ! उसमें से भी नौ महीने.....
‘‘एक पत्र तुम भी उसे लिख देना, ’’ कहती हुई मां अलमारी में से अपने कपड़े़ लेकर बाहर चली गयी हैं और मुझे एक और खूँटे से बाँध गयी हैं।
कागज लेकर बैठता हूँ पर हाथ ही नहीं चलते। क्या लिखना ठीक होगा। यह कि मैं खुश हो रहा हूँ या मुझे बहुत ही अटपटा लग रहा है या कि हम सब, मेरा मतलब है माँ पापा बहुत ही खुश हैं। नहीं, नहीं, यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि अब तो तुम सच में बड़ी हो गयी हो। तुम्हें बधाई देता हूँ। मन से।
शब्द खोखले लगते हैं। बजते हुए ! उछाह और प्रवाह के बिना। यहाँ से कुछ चलेगा ही नहीं तो पहुँचेगा कैसे ! यह व्यायाम व्यर्थ होगा। उसे आशा ही कहाँ होगी कि मेरा पत्र आएगा ! वह देना पाना हमारे बीच बना ही कब था ! उस पारस्परिकता ने जन्म ही कहाँ लिया जबकि उस काल में वही सबसे स्वाभाविक बात रही होती। कहने को हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे, एक ही दरवाजे से घुसते-निकलते थे। एक ही दिनचर्या के अधीन रखे जाते थे। पर.....
एक तटस्थ-सा भाव उसके लिए मेरे मन में क्यों रहा,. इसे मैं आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। मौसी यानी माँ की चचेरी बहन की लड़की की तरह उसने इस घर में अचानक प्रवेश पाया था। मैं तब सातवें या शायद आठवें में था।
अपने उस एकान्त में एक साथी पा जाने की मुझे कोई खाश खुशी नहीं हुई थी। न नकार। शायद तब तक मेरे आसपास सबकुछ तय हो चुका था। मेरे खेल और मेरी रुचियाँ अपनी परिधि टटोलकर अपने मनचीते केन्द्रों में स्थिति हो चुकी थीं। रुचियों का पुल उसके मेरे बीच नहीं बन पाया था।
उसकी खाट मेरे कमरे में बिछा दी गयी थी। वह मेरे साथ स्कूल जाने लगी थी। मेरे साथ खाना खाने लग गई थी। पता नहीं कहाँ से पा गये उत्साह से माँ मुझे उधर ठेलने लगी थी। मेरे लिए उस साहचर्य की जरूरत और सघनता को माँ ने स्वयं तय कर लिया था। उतनी ही ललक और उत्साह से मैं प्रस्तुत न हो पाऊँ तो माँ कुपित होने लग गयी थी वह क्यों मेरे साथ बैडमिण्टन खेलने नहीं जा रही थी। उसे तैरने ले जाने में मुझे क्या तकलीफ है जबकि पापा ने क्लब के कार्ड में उसका नाम बढ़वा लिया है....मैं क्यों उसकी रुचियों और रुझानों के विकास पर कोई ध्यान नहीं देता। जबकि मैं उससे बड़ा हूँ..,...।
याद करूँ तो मेरे आसपास जो संसार था, उसमें इस अचानक के प्रवेश का कोई स्थान नहीं था। कुछ भी मेरे मन में साफ नहीं था। न उस पर अपने अधिकार के बारे में, न उसके प्रति अपने कर्तव्य को लेकर। माँ मुझे टोकतीं। ताड़ना देतीं। वंचित करतीं। अपना पुत्र होने की अतिरिक्तता को मुझसे छीन-झपट कर उसके हवाले कर देना चाहतीं। याद नहीं पड़ता- माँ ने उसे कभी खास डाँटा-फटकारा हो। मुझे तो ठीक से यह भी अनुमान नहीं था कि माँ की डाँट-फटकार के प्रति उसकी सहिष्णुता थी कितनी !
आज सोचता हूँ, माँ क्यों करती थी ऐसा। बड़ी–छोटी उँगली को खींच-खाँच कर बराबर कर देना चाहती थीं। ऐसा होता है क्या ? हो सकता है क्या ? वह भी एकाएक बीच में। बिना किसी स्पष्ट कारण या तैयारी के।
आत्मगरिमा को पाने का, या अपनी ही न्यायप्रियता पर रीझने का माँ के पास शायद यही एक ढंग होगा। लगता होगा कैसे हँसते-हँसते वह किसी पराये को श्रेय दे देती हैं। अपने पर कठोर हो लेती हैं। ऐसा कितने लोग कर पाते हैं, करने की चेष्टा में फूहड़ हो जाते है, क्योंकि नैसर्गिक सम्बन्ध तो चुप रह सकता है, शिराओं में बजता है। ओढे़ हुए सम्बन्धों को जताना-प्रकटाना पड़ता है।
इन सब बातों ने भी उसके प्रति मेरी तटस्थता को धारदार ही बनाया होगा। माँ के दिए ममत्व को वह प्रकट प्रीति से भोगती थी। किशोरी से बच्ची बनने की कृत्रिमता को ओढ़ती थी। इतराती थी और ध्यान खींचते-खींचते केन्द में सरकती चली आती थी जबकि मुझे ‘अपनी उम्र से बड़ा’ कहकर अपने पैरों के नीचे की जमीन से बेदखल कर दिया जाता। ऐसा करते समय भी असल में वे ऐसे परिपक्क बच्चे के जन्मदाता होने के उपलक्ष्य में अपना ही अभिषेक कर रहे होते । मैं एक उदाहरण ! मैं एक अनूठा ! ‘‘भई, बड़ा ही धीरज है, कभी इस लड़के में न कोई अनुचित हठ...न शरारत !’’ अब लगता है, कभी हठ या शरारत की होती तो उन्हें आघात ही लगता।
इन बातों का कुछ खास बोझ पड़ता रहा हो, याद नहीं पड़ता। मुझे भी शायद यही अनुकूल पड़ता रहा होगा। दोस्तों के लम्बे झुण्ड मुझे उबाते हैं। यह ऊब निश्चय ही दोस्तों को भी मुझसे होती होगी, नहीं तो ‘चूजी’ कह-कहकर हर समय वे मेरा बहिष्कार करने की ताक में न रहते। इलाहाबाद में भास्कर और दिल्ली में बासू के सिवा अभी तक मेरा कोई अंतरंग दोस्त नहीं है। अकेलापन मुझे उबाता नहीं, बल्कि बहुत दिनों तक उपलब्ध न हो तो क्षुब्ध करता है।
उसके आने के बाद भी मुझे अकेला ही कहा जाए तो ठीक ही होगा। इस स्थिति का कष्ट न उसके आने के पहले था, न बाद में था। कष्ट कुछ था तो माँ के हाथ में पकड़ी लोहे की मापक छड़ का, जो हर चीज को एक ही सीध में मापना चाहती थी। अब वह इस घर में नहीं रहती। अपना कहे जाने वाले घर में रहती है।
एम.ए. और उसके बाद एल.एल.बी करके जब वह घर लौटा था तो वह मुझे एकाएक बड़ी जैसी लगी थी। गठन, उठान, उग्रता। माँ ने कहा था लड़कियाँ जल्दी सयानी हो जाती हैं- ब्याहने योग्य। उत्सुकता में मैंने उससे एक दिन पूछा था- ‘‘तुम्हें ठीक लगता है क्या इतनी जल्दी शादी-वादी का किस्सा ?’’ चूंकि मेरे लिए यह बात अकल्पनीय थी। कोई भी हम उम्र संगी-साथी, परिचित इस तैराकी के लिए तैयार नहीं था। प्राथमिक थी दिशा की तलाश। कैसे कोई बिना
सोचे ऐसे सागर में कूद जाए, जहाँ से कभी वापसी भी सम्भव नहीं।
मेरे प्रश्न से वह टँग-सी गयी- ‘‘कभी तो लगता है फालतू में बँध जाएँगे ! फिर लगता है बड़ा अच्छा लगेगा। कोई बिल्कुल अपना तो होगा।’’
मैं जैसे सन्नाटे में। वह हम लोगों को गाली दे रही थी। विशेष तो माँ को, जो उसको माँ देने के उत्साह में अपनी देह के रोएँ भी फूँक रही थी। मेरी प्रतिक्रिया पर उसका ध्यान नहीं था। वह अपनी रौ में थी।
‘‘कितना अजीब होता है न इतनी बड़ी दुनिया में कुछ भी अपना होना....कितना हताश करता है....’’ उदासी का एक चिथड़ा उसके उजले गालों को फटकारता निकल गया। मेरे सामने बैठी इस समय वह मुझे ऐसी लगी थी जैसी कभी लगती नहीं थी-अन्तरंग, आर्द्र, उदास।
‘‘क्यों मौसी तो हैं न, वह...’’
‘‘ऊँह !’’ उसने मुझे अधबीच टोक दिया था, ‘‘तुम मेरी मम्मी की बात कर रहे हो न ? मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके लिए। जब जहाँ चाहा, ठेल दिया। मेरी पढ़ाई-लिखाई की बात को प्रमुख बनाकर....’’
‘‘तुम गलत कहती हो ! सुना तो यह है कि तुम्हारे कारण उन्होंने अपना दुःख-सुख नहीं देखा। जबकि चाहतीं तो फिर अपना घर बसा सकती थीं।’’
‘‘उसमें अभी क्या कमी है। स्कूल की वह छोटी-छोटी छोकरियाँ उन्हें ज्यादा प्यारी लगती हैं, क्योंकि हर समय आसपास मँडराती रहती हैं। यह मुझसे नहीं होता। तुम्हें नहीं पता बड़ी काइयाँ हैं ये लड़कियाँ खूब फुलाना-फुसलाना जानती हैं। दे नो हाउ टु फीड हर ईगो। टु गेट द बेस्ट आउट ऑफ हर। ...और मम्मी भी उनकी बातों में आ जाती हैं। तुम्हें एक बात बताऊँ....’’
वह पलँग के परले सिरे से सरककर मेरे निकट आ गयी थी, जैसे कोई बड़े भेद की बात कहने जा रही हो-‘‘सच तो यह है कि वह मुझे कभी अपनी माँ ही नहीं लगतीं। कुछ कहते रहो, कभी नहीं समझतीं ! बस, हर समय पट्टी-स्लेट लेकर बैठे रहो छोकरियों से बतियाते रहो। मन से उनसे मेरी एक मिनट को नहीं बनती। काश ! मेरी भी तुम्हारे जैसी माँ होती....’’
‘‘है तो सही। वह तुम्हारी भी तो माँ हैं।’’ –मैं द्रवित हो गया था।
‘‘नहीं ! वह तुम्हारी माँ हैं, मेरी माँ नहीं। आण्टी तो आण्टी ही होती हैं। ’’
गड्ड-मड्ड-सा उसका चेहरा एकाएक मुझे पिघला-सा लगा था। मैं अस्थिर हो गया था। अभी एक तो मैं अपनी ही दुखती रगों को जानता था।
क्या विडम्बना थी, उसके कारण मेरी माँ भी छिनती है और मेरी माँ उसे अपनी माँ भी नहीं लगती...पर उस समय तो मैं उसकी संजीदगी से ही आन्दोलित था। पता ही नहीं वह कैसे भूली-सी उस कगार पर आने लगी थी। वैसी अपनापे-भरी बात उसने मुझसे पहली बार कही थी-अन्तरंग तरीके से। ज्यादातर वह असहज और प्रतिक्रिया प्रधान मुद्रा में रहती है। रिश्तों के प्रति अनादर से भरी।
मैं सोच में पड़ गया था। क्षणिक ही सही, पर क्या चीज थी जो उसे इस अन्तरंगता के क्षण तक ला सकी थी। इस पुल को न बनने देने में क्या कहीं मैं भी दोषी था ?
ससुराल चली जरूर गयी थी फिर भी जैसे इसी घर में थी। कभी इस कारण तो कभी उस करण से माँ की चिन्ताओं के घेरे में। जाने किस सजातीय साँकल से बँधी। जिन दिनों मैं एम.ए. के लिए इलाहाबाद चला गया था, उन दिनों उसका रिश्ता माँ से गहरा हुआ होगा। मैं वैसे भी सदा हाशिये पर ही बना रहता था। एक तो मैं उद्घोषित चुप्पा ! फिर एक के बाद दूसरी परीक्षाओं का भार ! कुछ अपनी ही स्थिति और स्वप्र के बीच के तनाव। मैं जैसे घर में होता ही नहीं था।
‘‘अच्छा, तुम बताओ, जाना चाहिए न ? अभी तो उसकी डिलीवरी से निपटकर आयी हूँ ! ’’माँ ने कमरे में घुसते ही अपनी दुविधा पसार दी।
‘‘पर कहाँ ?’’
‘‘अरे, ऑपरेशन हुआ है न उसका। रमण की चिट्ठी आयी है।’’
‘‘कैसा ऑपरेशन.....किसका ऑपरेशन....?’’
माँ को अपनी भूल पता लगती है। बात के सभी छोर अभी तो उसकी मुट्ठी में ही हैं। ‘‘अब तुम्हें क्या बताऊँ, उसकी छाती में.....मेरा मतलब है उसके ब्रेस्ट में गिल्टी प़ड़ गयी थी। मवाद भर गया था। काफी गहरा काटना पड़ा !’’
‘‘कैन्सर है क्या ?’’ मैं काँप जाता हूँ।
‘‘ऊह ! कैन्सर कहाँ से हो जाता है अकसर ऐसा, बच्चे को दूध नहीं पिलाया होगा। अब तू....’’
माँ संकोच में हैं। इतना भी वह पता नहीं कैसे बोल गयीं। शायद चिन्ता का तार उसके मन में अभी टूटा नहीं है। पापा के कहने पर यह बात स्पष्ट हो गयी है।
‘‘यह अब नया चला है, ’’ पापा का नाश्ता रखते माँ बोलती जाती हैं। ‘‘तुम्हें मालूम है, ऐसा क्यों हुआ....बच्चों को दूध पिलाने से इनकी फिगर बिगड़ती है न....।’’
मेरे कान खड़े हो जाते हैं। ‘‘अब जैसे नहीं बिगड़ेगी इस काटपीट से। फैशन के मारे मरी जाती हैं ये लड़कियाँ !’’
कुछ-कुछ साफ होने लगता है मन में। कड़ियाँ जुड़ती हैं। वह ऐसी ही मिट्टी की बनी हैं। उमगायी ललसायी हुई। जीवन को चाँपकर रखने के चाव से भरी हुई। अपनी जरूरतों के प्रति एकदम चटक चौकन्नी। माँ को यह ललक डराती थी। उसकी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में की आत्मनिर्भरता को जरूरी समझते हुए भी उसके हाथ पीले कर देना चाहती थी।
पढ़ने जैसा पराक्रम का उसे शौक नहीं था, और मैं था कि एक तरह की पुस्तकों से ऊबने पर दूसरी तरह की पुस्तकों में डूबता था। केवल सन्दर्भ और विषय बदल जाते। थुल-थुल रेत में खड़ी पाठ्यक्रम की नाव मेरे लिए सदा विविध प्रसंगों वाली नदी में खुलती।
वह अकसर आँगन में तसला रखकर पैर भिगोये बैठी रहती। फिर उन्हें पोंछती। फिर क्रीम लगाती। मुँह रगड़ती। कपड़े सभाँलती। बार-बार शीशा देखती। पलंग पर पसरकर छत देखती रहती। मेरी तरह नहीं कि एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक से तीसरी ! तीसरी से डायरी। फिर किताब, फिर कॉपी, फिर ‘पजल’ फिर स्टीरियो। मक्खी की तरह मुझे इधर से उधर कूदते देख वह मेरी खिल्ली-सी उड़ाती। होठों में बन्द एक तरेर जैसी उसके चेहरे पर छाप जाती। पलँग पर पैर लटका कर अपनी ठुड्ढी के नीचे दोनों हाथ टेककर वह अपनी आँखों को जिधर जिधर मैं जाता, उधर घुमाती रहती।.... ऐसा आमोद से भरा फुर्सती-सा उसका अन्दाज !
अकसर किसी कॉमिक्स या किताब को बेध्यान-सा होकर उठाती और पढ़ने लगती। पूरा डूब जाती, पर यह डूबना उसमें और अधिक डूबने का उत्साह पैदा कर दे, ऐसा बन नहीं पाता था। पुस्तक को ऐसे निवृत्त भाव से किनारे रखती जैसे किसी अटपटे काम को कर लेने के बाद आराम जरूरी हो।
क्यों उसमें वह बेचैनी पैदा नहीं होती थी, जो उसके समवयस्कों को हर समय पंजे पर खड़ा रख सकती थी।
वह अपने को खाली और खुला छोडे़ रखती, ऐसे जैसे कहीं कुछ होने को है कोई अचम्भा जैसा घट जाने को है। यह व्याख्या भी मुझे आज सूझ रही है। तब तो उसे यूँ पड़े-पड़े छत ताकने या पैर हिलाते देख खीझ चढ़ जाती थी।
‘‘इतनी किताबें लाकर देता हूँ लायब्रेरी से पढ़ती क्यों नहीं ?’’
ऐसे जवाब-तलब का उसने अकम्प उत्तर दिया था-‘‘नहीं पढ़ती तुम्हें क्या नम्बर तो कम नहीं आते !’’
‘‘नम्बर तो सबक घोंट कर भी आ जाते हैं, पर इससे ज्यादा क्या कुछ जानना नहीं होता ?’’
उसका चेहरा वैसा ही- उद्धत, आत्मतृप्त। भर्त्सना की नोक को मेरी ओर घुमाता हुआ- ‘‘अच्छा बस ! तुम्हें किताबें चाटनी हैं तो चाटो। मैं तो अभी बासू आएगा तो उसके साथ बैठकर शतरंज खेलूँगी।
उफ्फ ! बासू...बासू !.....बासू ! मेरे लिए भी तो वही एक था। वही एक अकेला।
परिचितों की भीड़ को काटता, किसी सुभग घड़ी वह मुझ तक चलता चला आया था और मेरी बगल में खड़ा हो गया था। इस तलाश का श्रेय भी उसे ही था। मेरे लिए तो वह ‘यह नहीं’, ‘यह भी नहीं’ के दम्भी नकार को चकनाचूर कर देने वाला एक अनूठा चमत्कार था।
वह था तो बस था, जैसे हजारों विखण्डित चीजें इस ब्रह्माण्ड में घूमती हैं और अपने पूरेपन को पा लेने के लिए किसी परिचित परिक्रमा-पथ में घुस लेती हैं। हार्दिकता के सत्त्व को उकेर लेती हैं।
मैं खिंचता आया था या बासू, नहीं जानता। मित्र पा जाए, ऐसा आन्तरिक संकट उसके जैसे व्यक्ति को क्योंकर रहा होगा। वह तो अकेला रह सकता था। रह तो मैं सकता था पर उसके और मेरे अकेलेपन में फर्क था अनवरत अशान्त था। वह आत्म-सम्पन्न। मैं एक से दूसरी से तीसरी व्यस्तता में अपने को बींध कर पहले ही प्रतिबन्धित और सुरक्षित कर लेता था। वह बेपरवाह था-फक्कड़ और मुक्त। जहाँ बैठ गया वहीं पर पूरा। वह सब कहीं जम सकता था। उसका सब कहीं प्रवेश था- हर किस्म की टोली में। बलियाटिक्स और बीटल्स, हिप्पी और हारे, अगुए और पिछलगुए- सबके साथ। सबमें रहते हुए भी वह अपने स्वत्व को अछूता रख लेता था। कोई कच्चापन कहीं दीखता तभी न कोई उसे छोड़ता। उसके मन तक पहुंचने के लिए उसकी निहायत उत्कट और उदग्र दृष्टि के सामने से गुजरना पड़ता था। वह सामना किसी भी प्रकार के आश्वासन से खाली होता था, रूखा-सूखा, असान्त्वनीय। जो कोई इस खुरदरेपन को झेल सकता होगा, वही तो उसकी आन्तरिकता तक पहुँचेगा।
मैं जाने क्यों, उसी को लेकर बहक रहा हूँ। क्या वह मेरे भीतर इतना खुला हुआ, इतना विद्यमान है कि अपनी अनुपस्थिति को भी अपनी मनोमयता में तब्दील कर दे सकता है। उन दिनों के बाद मुझे उसका कोई अता-पता नहीं। पूरे दो वर्ष....।
पिछले सप्ताह ‘एक्सप्रेस’ के तीसरे पन्ने पर उसकी फोटो देखी थी। दिल्ली कन्याकुमारी तक जाने वाली टोली के अगुआ के रूप में। अचम्भा नहीं हुआ था। यह दल उसी ने तैयार किया होगा। इतनी उर्जा उसके भीतर है। बल्कि इसलिए इतनी आतंककारी उदग्रता उसमें है। उसे ऐसा कुछ करते देखकर लगता है कि ऊर्जा के इस अक्षय आवेग में खपत हो जाना अच्छा है। यह उसके हित में है। उसके सामान्य हो सकने के लिए जरूरी है।
चाहे यह बहस उसकी सदा-सदा जारी रहा करती थी कि हम सब क्यों सदा साधारण-सामान्य के हक में बने रहते हैं। हर नये संयोजन के विरुद्ध अडे़ रहते हैं। यह काम फिर जबरजस्ती कोई साधारण व्यक्ति या परिस्थिति हमसे करवाती है।
‘‘तुम्हें मालूम है विशाल, हम ऐसा क्यों करते हैं ? असाधरणता हमें हमेशा आतंकित करती है क्योंकि तुलना में अपने को हलका और पुराना सिद्ध करके फेंक देती है।’’
आश्चर्य जरूर है कि मैं उसके साथ ऐसी किसी आतंककारी अनुभूति से क्यों कर बच गया था। मिलते ही मुझे लगा था कि वह मेरे ही अस्तित्व का एक जरूरी हिस्सा है, जिसे सामने रखकर मैं अपनी अब तक की तलब और तड़प के स्वभाव को जान पा सकता हूँ। बिना यत्न के स्वत्व तक पहुंच और पहुँचा रहा हूँ। उससे वह बातें होती थीं, सदियों से भीतर तन्द्रिल पड़ी हैं ...पात्र को पाकर जागेंगी नहीं तो अव्यक्त रह जाएँगी, क्योंकि उन कोषों का कोई सिद्ध व्यावहारिक पक्ष तो नहीं होता।
आश्चर्य यह भी है कि हम दोनों एकदम अलग-अलग मिट्टी के बने थे। मैं यदि दुबला, कुछ-कुछ नाजुक, चिड़चिड़ा, अतिरिक्त संवेदनशील, अन्तर्मुखी और भावुक हूँ तो वह पुरुषों का भी पुरुष, मांसल, युक्त और आत्माश्वस्त। एकदम विपरीत। हमारा सम्बन्ध ऐसा, जैसे दो बाँसों के बीच बँधी रस्सी का साफ-सुथरा तनाव। एक-दूसरे का अकृत्रिम स्वीकार।
जोखिम की हदों से टकराता साहस उसमें कहाँ से आता है, मैं जल्दी नहीं समझ सका। कभी माँ-बाप के प्रसंग के माध्यम से उसकी जड़े़ टटोलने की कोशिश की तो उसने झटक दिया-बेरहमी से। यह जताते हुए कि वहाँ जाना बेकार है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i