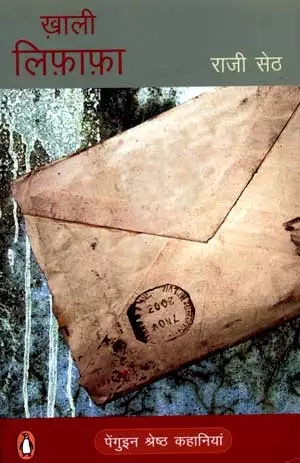|
कहानी संग्रह >> भारतीय कहानियाँ 1987-88 भारतीय कहानियाँ 1987-88राजी सेठ
|
358 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है 1987-88 की श्रेष्ठ कहानियों का संग्रह
Bhartiya Kahaniyan 1987-88
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रस्तुति
लगभग सात साल पहले भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रतिवर्ष प्रकाशित विभिन्न भारतीय भाषाओं में कहानी और कविता की प्रतिनिधि रचनाओं के अलग-अलग संकलन प्रकाशित करने की योजना बनायी थी। इन श्रृंखलाओं का प्रारम्भ 1983 में प्रकाशित कहानी और कविताओं से हुआ। शीघ्र ही इस प्रकार की अन्य विधाओं की चयनिकायें भी प्रकाशित करने का विचार है। कहानी और कविताओं की चयनिकाओं का साहित्यिक क्षेत्रों में जो स्वागत हुआ है उससे हमारी योजना को प्रोत्साहन मिला है। प्रस्तुत पुस्तक कहानी श्रृंखला की 5 वीं चयनिका है जिसमें दो वर्ष -1987 व 1988 की कहानियों को सम्मिलित किया गया है।
इससे पहले हर वर्ष की एक चयनिका होती थी। इस बार एक चयनिका में 2 वर्षों में प्रकाशित कहानियों को लेने का विशेष कारण है। वर्ष 1985 व 1986 की चयनिकाएँ काफी विलम्ब से प्रकाशित हुईं। 1986 से सम्बन्धित पुस्तक इस वर्ष (1990) मार्च में ही प्रकाशित हो पायी। कई क्षेत्रों में इस विलम्ब की आलोचना हुई; इसको अनुचित नहीं कहा जा सकता। यद्यपि इस प्रकार की चयनिकाओं के प्रकाशन में काफी समय उन बातों पर लग जाता है जिन पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं होता फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस विलम्ब में हमारा भी हाथ था। इतने विलम्ब से प्रकाशित इस प्रकार की चयनिकाओं का महत्त्व कम हो जाना स्वाभाविक है। अतः अगले वर्षों की चयनिकाओं को यथासम्भव समय से प्रकाशित करने के लिए काफी बे-मन से यह निर्णय लेना पड़ा कि एक संयुक्त चयनिका में 1987 व 1988 दोनों वर्षों की कहानियों को संकलित करके इसी वर्ष (1990) में प्रकाशित कर दिया जाय। साथ ही 1989 का संकलन 1991 के मध्य तक और 1990 का संकलन 1991 के अन्त तक निकालने का पूरा प्रयत्न किया जाये। हमें आशा है कि इन चयनिकाओं के प्रकाशन में जो लेखक व समीक्षक हमारे साथ जुड़े हैं उनका हमें पूरा सहयोग मिलेगा जिससे हमारा यह प्रयत्न सफल हो सके। यह भी स्पष्ट कर दूँ कि अनावश्यक विलम्ब को दूर करने के लिए इस चयनिका में केवल 13 भाषाओं की रचनाएँ ही दी गयी हैं। हर सम्भव प्रयत्न के बावजूद हमें कश्मीरी कहानियाँ नहीं प्राप्त हो सकीं। तीन लेखकों के परिचय के अप्राप्य रहने पर भी हमें प्रकाशन में और अधिक विलम्ब करना उपयुक्त नहीं लगा। भविष्य में इस प्रकार की कमियाँ न हों यह निश्चय ही हमारा प्रयत्न रहेगा।
इस चयनिकाओं के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न बराबर दोहराये जा रहे हैं। उनका फिर से उत्तर देना आवश्यक लगता है। एक प्रश्न तो भाषाओं को लेकर है। कुछ समीक्षकों ने मणिपुरी, मैथिली, राजस्थानी, डोंगरी आदि की रचनाओं के सम्मिलित न किये जाने की आलोचना की है। इस पर हमें कुछ आश्चर्य होता है। यह कोई नयी बात नहीं कही गयी है। जब पहली बार यह आपत्ति उठायी गई थी तो यह स्पष्ट किया गया था कि हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के अनरूप इन चयनिकाओं का क्षेत्र भी भारतीय संविधान के 8वें परिशिष्ट में उल्लिखित 15 भाषाओं तक ही सीमित रखा है। (संस्कृत में आजकल कहानियाँ नहीं लिखी जातीं इसलिए एक चयनिका में 14 भाषाओं की 28 कहानियाँ दी जाती हैं)। यह एक नीतिगत निर्णय है जिस पर किसी विवाद की गुंजाइश नहीं लगती और इसमें फिलहाल परिवर्तन करने का हमारा कोई विचार नहीं है। दूसरी बात कहानियों के चयन की है। मुख्यतः प्रश्न यही उठाया जाता है कि इन कहानियों को उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ किस आधार पर माना जाय। यह तो स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई भी चयन निर्णय पूर्णतः सन्तोषप्रद नहीं हो सकता। यह भी ठीक है कि किसी भी भारतीय भाषा से एक वर्ष में दो से अधिक अच्छी कहानियाँ छाँटी जा सकती हैं; वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक भाषा में हर वर्ष दो से कहीं अधिक अच्छी कहानियाँ चुनी जा सकती हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि एक चयनिका में उन सबका संकलन करना व्यावहारिक नहीं हो सकता। इसलिए इस योजना में सभी भाषाओं के प्रति एक भाव की दृष्टि रखते हुए केवल दो-दो कहानियाँ ही सम्मिलित करने की बात तय की गयी थी। इन कहानियों के सर्वश्रेष्ठ होने का दावा हमने कभी नहीं किया। हाँ अच्छी, प्रतिनिधि कहानियाँ यह अवश्य हैं।
इसी सन्दर्भ में इस योजना में अन्तर्निहित एक परिकल्पना की चर्चा और कर दूँ। जैसा मैंने ऊपर कहा यह चयनिकाएँ भारतीय भाषाओं की सभी उत्कृष्ट और/या प्रतिनिधि कहानियों के संकलन नहीं हैं। जब यह योजना प्रारम्भ की गयी थी तभी एक विदेशी रेडियो का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ था। उनसे एक भेंट-वार्ता में मैंने स्पष्ट किया था कि एक वर्ष में एक भाषा की केवल दो कहानियों का इस रूप में प्रकाशन शायद अभी बहुत अर्थपूर्ण न लगे पर 7-8 चयनिकाओं के प्रकाशन के बाद भारतीय साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन और कहानी साहित्य की नयी प्रवृत्तियों को समझने के लिए यह संकलन अवश्य ही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ ग्रन्थ होंगे। आज जब हमारे विश्वविद्यालयों में भारतीय साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन को पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए बल दिया जा रहा है, मेरी यह धारणा दृढ़ होती जा रही है। लेकिन मुझको यह लगता है कि इस आलोचना के पीछे एक भावना यह भी है कि हमारी चयन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं। निर्भर तो हमें सदा हर भाषा के चयनकर्ता पर ही रहना होगा। पर जहाँ अभी तक हम उससे वर्ष में प्रकाशित केवल दो कहानियाँ माँगते रहे हैं, भविष्य में दो से अधिक कहानियाँ मँगवायेंगे जिनमें से सम्पादक दो कहानियों का चयन कर लें। सम्पादन का दायित्व भी एक व्यक्ति से अधिक का होगा। प्रस्तुत चयनिका में यह इसलिए सम्भव हो सका है क्योंकि बहुत-सी भाषाओं की सन् 1987 व 1988 के लिए प्रस्तुत की गयी हमें कुल मिलाकर दो से अधिक कहानियाँ उपलब्ध थीं जिनमें से इस संकलन के लिए अन्तिम चयन किया गया है। हम समझते हैं कि वांछित सुधार की दिशा में यह सही कदम है और भविष्य में यह प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ होगी।
हमसे एक प्रश्न प्रायः और पूछा जाता है। कुछ समीक्षक और पाठकों को इस पर आश्चर्य है कि शीर्षस्थ कथाकारों की कृतियाँ इसमें स्थान क्यों नहीं पातीं। उत्तर स्पष्ट है कि हो सकता है वर्ष विशेष में इन शीर्षस्थ लेखकों की कोई रचना पहली बार प्रकाशित ही न हुई हो और यदि हुई भी हो तो उसकी तुलना में अन्य लेखकों की कृतियाँ इस संकलन के लिए अधिक उपयुक्त हों। पाठकों को सम्भवतः स्मरण होगा कि पिछले संकलनों में कई बार ऐसी कहानियाँ सम्मिलित की गयी हैं जो उनके लेखकों की पहली कृतियाँ थीं। इस बार कुछ शीर्षस्थ कथाकारों की कहानियों की संस्तुति की गयी थी पर स्वयं चयन-कर्ताओं से परामर्श करने के बाद उदीयमान लेखकों की अधिक सशक्त और सुन्दर कहानियों को चुनना अधिक उचित लगा। ऐसी स्थिति में केवल नाम के आधार पर शीर्षस्थ कहानीकार की कहानी इस संकलन में सम्मिलित करके हम अपनी योजना व पाठकों के साथ अन्याय नहीं करना चाहते।
इस प्रकार की चयनिका की सफलता के लिए साहित्यिक बिरादरी के सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें जिस प्रकार यह सहयोग मिल रहा है उससे हम अभिभूत हैं। हम अपने चयन मण्डल के सदस्यों, लेखकों, व उन सभी स्त्रोतों के आभारी हैं जिनके सहयोग से इस चयनिका का संकलन संभव हुआ है। हिन्दी की प्रख्यात कथा लेखिका श्रीमती राजी सेठ ने इस चयनिका के सम्पादन में विशेष योगदान किया है। लेकिन उनके स्नेह को ध्यान में रखकर उनके प्रति आभार प्रकट या धन्यवाद ज्ञापन करना मुझे बहुत हल्का लगता है।
इस पुस्तक की इतनी सुरुचिपूर्ण साज-सज्जा के लिए कलाकार पुष्पकणा मुखर्जी व सुन्दर छपाई के लिए तोषी जैन के प्रति आभार व्यक्त करने में मुझे प्रसन्नता है। और अन्त में ज्ञानपीठ परिवार के अपने सहयोगियों चक्रेश जैन, नेमिचन्द्र जैन, सुधा पाण्डेय व चन्द्रप्रकाश मित्तल की सहायता के लिए कृतज्ञता प्रकट करना मेरे लिए केवल औपचारिकता नहीं है।
इससे पहले हर वर्ष की एक चयनिका होती थी। इस बार एक चयनिका में 2 वर्षों में प्रकाशित कहानियों को लेने का विशेष कारण है। वर्ष 1985 व 1986 की चयनिकाएँ काफी विलम्ब से प्रकाशित हुईं। 1986 से सम्बन्धित पुस्तक इस वर्ष (1990) मार्च में ही प्रकाशित हो पायी। कई क्षेत्रों में इस विलम्ब की आलोचना हुई; इसको अनुचित नहीं कहा जा सकता। यद्यपि इस प्रकार की चयनिकाओं के प्रकाशन में काफी समय उन बातों पर लग जाता है जिन पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं होता फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस विलम्ब में हमारा भी हाथ था। इतने विलम्ब से प्रकाशित इस प्रकार की चयनिकाओं का महत्त्व कम हो जाना स्वाभाविक है। अतः अगले वर्षों की चयनिकाओं को यथासम्भव समय से प्रकाशित करने के लिए काफी बे-मन से यह निर्णय लेना पड़ा कि एक संयुक्त चयनिका में 1987 व 1988 दोनों वर्षों की कहानियों को संकलित करके इसी वर्ष (1990) में प्रकाशित कर दिया जाय। साथ ही 1989 का संकलन 1991 के मध्य तक और 1990 का संकलन 1991 के अन्त तक निकालने का पूरा प्रयत्न किया जाये। हमें आशा है कि इन चयनिकाओं के प्रकाशन में जो लेखक व समीक्षक हमारे साथ जुड़े हैं उनका हमें पूरा सहयोग मिलेगा जिससे हमारा यह प्रयत्न सफल हो सके। यह भी स्पष्ट कर दूँ कि अनावश्यक विलम्ब को दूर करने के लिए इस चयनिका में केवल 13 भाषाओं की रचनाएँ ही दी गयी हैं। हर सम्भव प्रयत्न के बावजूद हमें कश्मीरी कहानियाँ नहीं प्राप्त हो सकीं। तीन लेखकों के परिचय के अप्राप्य रहने पर भी हमें प्रकाशन में और अधिक विलम्ब करना उपयुक्त नहीं लगा। भविष्य में इस प्रकार की कमियाँ न हों यह निश्चय ही हमारा प्रयत्न रहेगा।
इस चयनिकाओं के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न बराबर दोहराये जा रहे हैं। उनका फिर से उत्तर देना आवश्यक लगता है। एक प्रश्न तो भाषाओं को लेकर है। कुछ समीक्षकों ने मणिपुरी, मैथिली, राजस्थानी, डोंगरी आदि की रचनाओं के सम्मिलित न किये जाने की आलोचना की है। इस पर हमें कुछ आश्चर्य होता है। यह कोई नयी बात नहीं कही गयी है। जब पहली बार यह आपत्ति उठायी गई थी तो यह स्पष्ट किया गया था कि हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के अनरूप इन चयनिकाओं का क्षेत्र भी भारतीय संविधान के 8वें परिशिष्ट में उल्लिखित 15 भाषाओं तक ही सीमित रखा है। (संस्कृत में आजकल कहानियाँ नहीं लिखी जातीं इसलिए एक चयनिका में 14 भाषाओं की 28 कहानियाँ दी जाती हैं)। यह एक नीतिगत निर्णय है जिस पर किसी विवाद की गुंजाइश नहीं लगती और इसमें फिलहाल परिवर्तन करने का हमारा कोई विचार नहीं है। दूसरी बात कहानियों के चयन की है। मुख्यतः प्रश्न यही उठाया जाता है कि इन कहानियों को उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ किस आधार पर माना जाय। यह तो स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई भी चयन निर्णय पूर्णतः सन्तोषप्रद नहीं हो सकता। यह भी ठीक है कि किसी भी भारतीय भाषा से एक वर्ष में दो से अधिक अच्छी कहानियाँ छाँटी जा सकती हैं; वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक भाषा में हर वर्ष दो से कहीं अधिक अच्छी कहानियाँ चुनी जा सकती हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि एक चयनिका में उन सबका संकलन करना व्यावहारिक नहीं हो सकता। इसलिए इस योजना में सभी भाषाओं के प्रति एक भाव की दृष्टि रखते हुए केवल दो-दो कहानियाँ ही सम्मिलित करने की बात तय की गयी थी। इन कहानियों के सर्वश्रेष्ठ होने का दावा हमने कभी नहीं किया। हाँ अच्छी, प्रतिनिधि कहानियाँ यह अवश्य हैं।
इसी सन्दर्भ में इस योजना में अन्तर्निहित एक परिकल्पना की चर्चा और कर दूँ। जैसा मैंने ऊपर कहा यह चयनिकाएँ भारतीय भाषाओं की सभी उत्कृष्ट और/या प्रतिनिधि कहानियों के संकलन नहीं हैं। जब यह योजना प्रारम्भ की गयी थी तभी एक विदेशी रेडियो का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ था। उनसे एक भेंट-वार्ता में मैंने स्पष्ट किया था कि एक वर्ष में एक भाषा की केवल दो कहानियों का इस रूप में प्रकाशन शायद अभी बहुत अर्थपूर्ण न लगे पर 7-8 चयनिकाओं के प्रकाशन के बाद भारतीय साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन और कहानी साहित्य की नयी प्रवृत्तियों को समझने के लिए यह संकलन अवश्य ही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ ग्रन्थ होंगे। आज जब हमारे विश्वविद्यालयों में भारतीय साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन को पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए बल दिया जा रहा है, मेरी यह धारणा दृढ़ होती जा रही है। लेकिन मुझको यह लगता है कि इस आलोचना के पीछे एक भावना यह भी है कि हमारी चयन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं। निर्भर तो हमें सदा हर भाषा के चयनकर्ता पर ही रहना होगा। पर जहाँ अभी तक हम उससे वर्ष में प्रकाशित केवल दो कहानियाँ माँगते रहे हैं, भविष्य में दो से अधिक कहानियाँ मँगवायेंगे जिनमें से सम्पादक दो कहानियों का चयन कर लें। सम्पादन का दायित्व भी एक व्यक्ति से अधिक का होगा। प्रस्तुत चयनिका में यह इसलिए सम्भव हो सका है क्योंकि बहुत-सी भाषाओं की सन् 1987 व 1988 के लिए प्रस्तुत की गयी हमें कुल मिलाकर दो से अधिक कहानियाँ उपलब्ध थीं जिनमें से इस संकलन के लिए अन्तिम चयन किया गया है। हम समझते हैं कि वांछित सुधार की दिशा में यह सही कदम है और भविष्य में यह प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ होगी।
हमसे एक प्रश्न प्रायः और पूछा जाता है। कुछ समीक्षक और पाठकों को इस पर आश्चर्य है कि शीर्षस्थ कथाकारों की कृतियाँ इसमें स्थान क्यों नहीं पातीं। उत्तर स्पष्ट है कि हो सकता है वर्ष विशेष में इन शीर्षस्थ लेखकों की कोई रचना पहली बार प्रकाशित ही न हुई हो और यदि हुई भी हो तो उसकी तुलना में अन्य लेखकों की कृतियाँ इस संकलन के लिए अधिक उपयुक्त हों। पाठकों को सम्भवतः स्मरण होगा कि पिछले संकलनों में कई बार ऐसी कहानियाँ सम्मिलित की गयी हैं जो उनके लेखकों की पहली कृतियाँ थीं। इस बार कुछ शीर्षस्थ कथाकारों की कहानियों की संस्तुति की गयी थी पर स्वयं चयन-कर्ताओं से परामर्श करने के बाद उदीयमान लेखकों की अधिक सशक्त और सुन्दर कहानियों को चुनना अधिक उचित लगा। ऐसी स्थिति में केवल नाम के आधार पर शीर्षस्थ कहानीकार की कहानी इस संकलन में सम्मिलित करके हम अपनी योजना व पाठकों के साथ अन्याय नहीं करना चाहते।
इस प्रकार की चयनिका की सफलता के लिए साहित्यिक बिरादरी के सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें जिस प्रकार यह सहयोग मिल रहा है उससे हम अभिभूत हैं। हम अपने चयन मण्डल के सदस्यों, लेखकों, व उन सभी स्त्रोतों के आभारी हैं जिनके सहयोग से इस चयनिका का संकलन संभव हुआ है। हिन्दी की प्रख्यात कथा लेखिका श्रीमती राजी सेठ ने इस चयनिका के सम्पादन में विशेष योगदान किया है। लेकिन उनके स्नेह को ध्यान में रखकर उनके प्रति आभार प्रकट या धन्यवाद ज्ञापन करना मुझे बहुत हल्का लगता है।
इस पुस्तक की इतनी सुरुचिपूर्ण साज-सज्जा के लिए कलाकार पुष्पकणा मुखर्जी व सुन्दर छपाई के लिए तोषी जैन के प्रति आभार व्यक्त करने में मुझे प्रसन्नता है। और अन्त में ज्ञानपीठ परिवार के अपने सहयोगियों चक्रेश जैन, नेमिचन्द्र जैन, सुधा पाण्डेय व चन्द्रप्रकाश मित्तल की सहायता के लिए कृतज्ञता प्रकट करना मेरे लिए केवल औपचारिकता नहीं है।
जेब घड़ी, हाथ घड़ी
मूल-सैयद अब्दुल मलिक
आजकल मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। व्यस्तता ही राजनीति है। हर तरफ बस कार्यक्रम ही कार्यक्रम हैं। किसी के साथ कुछ बातें करते रहने के समय भी उसे खुस करते, व्यग्र-अधीर, हड़बड़ाते रहना होता है। समय का एकदम ही अभाव हो गया है। बहुत सारे काम पड़े हैं। बहुत कुछ करने को पड़ा है। अनेक स्थानों पर जाना है। इस सबके अलावा विभिन्न संघों के प्रतिनिधि-मण्डलों के नाना प्रकार के आवेदन-अनुरोध, जनसमुदाय के नाना संघों की माँगें, शर्तें, प्रर्थनाएँ आदि तो हैं ही। ‘‘पेड़ जितना ही ऊँचा होता है, तूफानी हवा उतनी ही अधिक मात्रा में झकझोरती-कोंचती है।’’ अध्यापकीय-जीवन में लड़के लड़कियों को यह लोकोक्ति पढ़ाया करता था। अब इसकी यथार्थता को खुद ही महसूस कर रहा हूँ। आकाशवाणी से, जो थोड़ी देर के लिए समाचार प्रसारित होता है, उसे सुनते समय, उतनी जरा-सी वेला में ही, तीन-तीन बार उठकर जाना पड़ता है। किसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना, किसी के लिए किसी को दूरभाष (फोन) से बातें करना, किसी द्वारा किये गये फोन की बातें सुनना-कहां तक गिनाएँ ? काम का कहीं अन्त ही नहीं। रात बीती की न बीती, सबेरा हो पाया कि न हो पाया, कि नाना स्थानों से आये हुए लोगों-स्त्री-पुरुषों, युवकों-युवतियों-के आ इकट्ठा होने से मकान का मुख्य प्रवेश द्वार सामने का सारा प्रांगण, बरामदा, बैठक सभी कुछ भर उठता है। सभी लोगों की बाते सुननी पड़ती हैं, सभी को कुछ-न-कुछ सलाह परामर्श देनी होती है। कभी-कभी तो मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे आदमियों की भीड़ में ऊपर ही ऊपर बहा जा रहा हूँ। जैसे कि मेरी अपनी कोई निजी समस्या नहीं; दूसरों की समस्यायें ही मेरी समस्यायें हैं, अर्थात दूसरों की भावना चिन्ता, दूसरों का सर-दर्द मेरा सर-दर्द है।
मुझ जैसे आदमी के एक प्रदेश का एक मन्त्री बन जाना, कभी-कभी मुझे स्वयं ही एक अविश्वसनीय घटना जान पड़ती है। पहले ही विधायक (एम.एल.ए.) या मन्त्री होना बहुत बड़ी बात जान पड़ती थी। और क्या कहें ? किसी को विधायक या मन्त्री बनवाने के लिए निर्वाचन के समय मतदान का मत (वोट) जुटाने के लिए दौड़-धूप करना भी, एक विशेषतापूर्ण, अति-महत्त्वपूर्ण बात जान पड़ती थी, किन्तु अब तो मैं स्वयं ही एक मन्त्री हूँ। गणतंत्र में सभी कुछ सम्भव है। अन्यथा, यदि ऐसा न होता तो, मुझ जैसे एक गँवईं-गँवार के उच्च-माध्यमिक विद्यालय (हाई-स्कूल) के एक सहायक अध्यापक के किसी दिन मन्त्री बन जाने की घटना एक अविश्वसनीय बात ही समझनी पड़ती।
हाँ, इतना जरूर है कि अध्यायन कार्य करते हुए मैं थोड़ी-थोड़ी राजनीति भी नहीं करता रहा, ऐसा भी नहीं। हमारे इस देश में दुःखी, दरिद्र व्यक्ति ही राजनीति अधिक करते हैं। जिन दिनों मैं विद्यालय में अध्यापन करता था, उन दिनों माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक भी इन्हीं दुःखी-दरिद्रों की श्रेणी में आते थे। उन दिनों हमारा विद्यालय एक दैनिक समाचार-पत्र, एक या कि दो साप्ताहिक, पाक्षिक पत्रिका मँगवाया करता था। वही सब अध्यापकों के सामूहिक-कक्ष (कॉमन-रूम) की सार्वजनिक सम्पत्ति थी। उन्हें सभी पढ़ते थे। उनमें प्रकाशित कुछ बातों को लेकर सभी आपस में आलोचना-प्रत्यालोचना करते थे। कभी-कभी उन्हीं में से वे किसी विशेष बात को लेकर, या समाचार को लेकर आपस में तर्कातर्कि, वाद-विवाद करने में मशगूल हो जाते, इसी प्रकार के तर्कातर्कि, वाद-विवाद का दूसरा नाम है राजनीति। इस प्रकार की तर्कातर्कि, आलोचना-प्रत्यालोचना में मैं भी भाग लेता था। और विद्यालय के बाहर होने वाली साधारण जन सभाओं, सभा-समितियों में भी प्रायः योगदान करता था। अतएव वही सब कुछ राजनीति था।
उसके बाद तो फिर सचमुच की राजनीति में प्रवेश कर गया। एक राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य के रूप में जो आरम्भ किया तो क्रमशः एक स्थानीय छोटे नेता के स्तर तक ऊँचा उठ गया। उसके बाद तो सभा-समितियों, समारोहों के लिए प्रायः एक अपरिहार्य नेता ही हो गया। इस तरह मेरी कार्य व्यस्तता और मेरी महिमा काफी बढ़ गयी।
फिर उसके पश्चात् अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाने पर विधायक (एम.एल.ए) के निर्वाचन में प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ। निर्वाचन का खेल खेलने के लिए मेरे राजनीतिक दल ने भी पर्याप्त मात्रा में रुपया प्रदान किया। निर्वाचन या चुनाव के खेल को खेल कहना तनिक भी असंगत नहीं है। दरअसल, यह भी एक खेल ही है। इसमें भी (खेल प्रतियोगिता की भाँति) पक्ष है, विपक्ष है, दलबन्दी है, हार-जीत है। इस खेल के भी अपने नियम- निर्देश हैं। खेल के कला-कौशल, नियम-कायदों से अनभिज्ञ होने पर हार जाना ही स्वाभाविक है। हाँ, अन्य खेलों में साधारणतः दो दल या टीमें होती हैं, परन्तु निर्वाचन या चुनाव में यदा-कदा ही, कभी-कभार ही मात्र दो दल होते हैं। प्रायः कई-कई दल इस एक ही खेल को खेलने के लिए खेल-मैदान में उतरते हैं। पैरों से खेलने की गेंद, फुटबाल, गेंद और बल्ले का खेल, क्रिकेट, हाकी आदि खेलों में विजयश्री पाना या जीत प्राप्त करना निर्भर करता है खेलने वाले खिलाड़ी की कला-दक्षता पर। परन्तु हमारे देश, में निर्वाचन या चुनाव के इस खेल में विजयश्री या जीत प्रत्याशी के गुण-अवगुण पर निर्भर नहीं होती। मुख्य रूप से वह निर्भर करती है, रुपये पर। इसे देखकर ही निर्वाचन या चुनाव के इस खेल को बहुत से लोग ‘रुपये का खेल’ कहकर ही पुकारते हैं। दुःखी-दरिद्र, गरीब लोगों से भरे एक देश में भले ही ऐसी बात कहने का सुयोग नहीं है। परन्तु और कोई व्यक्ति इस बात को यदि स्वीकार न भी करे तो अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों से, अपने स्वयं भोगे हुए अनुभवों से मैं यह कह सकता हूँ कि इस बात में बहुलांश में, अधिकाधिक मात्रा में सच्चाई है। रुपया न होने से निर्वाचन या चुनाव नहीं होता। रुपया न होने पर हम विधायक (एम.एल.ए.), मन्त्री कुछ भी नहीं बन सकते।
मैंने भी निर्वाचन में क्या कोई कम रुपये खर्च किये ? हाँ, यह सच है कि खर्च करने के लिए मेरे पास अपना निजी संग्रहीत रुपया नहीं था। अध्यापकी कर-करके जो रुपये पा सका था, उससे तो महीना बिता पाना ही कठिन था। (घर के अत्यावश्यक खर्चों के लिए ही वह महीने भर को नहीं पोसाता था) इस तरह जो कुछ रुपये मैं कमा सका था, उसके हिसाब से एक निर्वाचन चुनाव लड़ने में खर्च होने वाले रुपये तो मैं तीन जन्मों में भी नहीं कमा सकता था। मेरे निर्वाचन में खर्च करने के लिए इतने अधिक रुपये कहाँ से, किस विधि से आये, यह एक खुली हुई अतिगोपनीय कहानी है।
निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए दल के प्रत्याशी चुन लिये जाने के बाद कुछ रुपये मैंने किसी-किसी से उधार में भी लिये थे। उस समय जिस किसी के पास भी रुपये थे, उनमें से किसी ने भी रुपये उधार देने से इनकार नहीं किया था। कुछ लोग तो ऐसे भी थे, जिनके पास यदि खुद का पैसा नहीं था, तो उन्होंने दूसरों से उधार लेकर मुझे रुपये दिये। मेरे अपने परिवार और नाते-रिश्ते के लोगों के अतिरिक्त मेरे विद्यालय के सहकर्मी सारे अध्यापकों ने भी अपनी-अपनी औकात के मुताबिक मुझे रुपये देकर मेरी सहायता की। और-तो-और यहाँ तक कि एक ही विद्यालय में पढ़ाने का काम करके जो अध्यापक सेवा-निवृत्त हो चुके थे उनमें से भी दो एक जनों ने मुझे रुपये दिये थे। जो स्वयं नहीं आ सकते थे, उन्होंने किसी और के हाथों रुपये भिजवा दिये थे।
रुपये देकर इसी प्रकार से सहायता प्रदान करने वाले सेवा निवृत्त एक अध्यापक थे श्री पुण्यकान्त नाथ। कुछ वर्षों पहले ही वे सेवा निवृत्त हुए थे। उन्होंने एक आदमी के हाथों मेरे निर्वाचन खर्च के लिए बीस रुपये पठवाये थे, उसी के साथ मेरी विजय के लिए शुभकामना प्रकट करते हुए एक छोटा-सा पत्र भी भेजा था-
‘‘तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ जिससे कि तुम्हारी विजय हो। विजयी होकर जनता की भलाई करोगे, ऐसी आशा रखता हूँ। यदि मेरे पास होता तो बढ़ाकर दो रुपये और पठाए होता। मेरी अवस्था तो जानते ही हो। आशा करता हूँ बुरा नहीं मानोगे।–पुण्यकान्त।’’
बहुत सम्भव है सभी लोगों के आशीर्वाद और शुभ-कामनाओं के भरोसे मैं निर्वाचन में विजयी हुआ (विधायक चुना गया) और सरकार में मन्त्री भी बन गया।
मन्त्री बन जाने के बाद धीरे-धीरे मैंने अनेक लोगों को उनके द्वारा दिये गये उधार, उनके रुपये वापस लौटा दिये। किसी-किसी ने उसे वापस लिया, अधिकांश ने नहीं लिया। उसके बदले में उन्होंने अपना कोई-कोई, यह या वह, काम करवा लिया। किसी के लिए नौकरी, किसी का तबादला, किसी को पदोन्नति, किसी के लिए लाइसेन्स, परमिट आदि मंजूर करवा लिया।
प्रायः सभी ने प्रसन्न मन से हँस-हँस कर कहा-‘‘अरे रुपये की भी कोई बात है ? हमारा रुपया जो व्यर्थ नहीं हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। इस तरह मेरे निर्वाचन की वेला में रुपये उधार देकर, बाद में मेरे द्वारा लौटाये जाने पर भी जिन महान व्यक्तियों ने उसे वापस नहीं लिया, उन लोगों को मैंने हृदय से अपना अत्यन्त उपकारकर्त्ता और शुभचिन्तक माना। ‘‘मछली चाहिए या कि झील चाहिए ?’’ इस तरह की लोकोक्तिपरक पिपासा पर वे सभी लोग झील लेने के पक्ष में थे। क्योंकि झील के अपने कब्जे में बने रहने पर आखिर मछली कहाँ भाग कर बचेगी ?’’
मन-ही-मन मैंने अत्यन्त हार्दिक आनन्द का अनुभव किया। (यह सब मुझे बहुत अच्छा लगा) निर्वाचन की लड़ाई जीतने के लिए जो तमाम सारे रुपये मैंने पाये थे, यदि वह सारा-का-सारा फिर से लौटा देना पड़ता, तो मन्त्री के रूप में जो रुपये कमा रहा था, उसमें से कई महीनों की कमाई का रुपया खर्च कर देने को मजबूर हो गया होता। और यदि सचमुच ही ऐसा कर देना पड़ा होता तो इतने कम समय के अन्दर राजधानी में मकान बनाने के लिए जमीन नहीं खरीद पाये होता, और उस पर यह तीन मंजिला भवन भी नहीं गढ़वा पाये होता, यहाँ तक कि नयी कार खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपना नाम भी रजिस्टर नहीं करवा सका होता।
मन्त्री को जन-साधारण में ख्याति प्राप्त करने के लिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए जनता के बीच घूमना-फिरना पड़ता है, दौड़-धूप करनी होती है। सभा-समितियों में भाग लेना, सभा-समितियों का आयोजन करना पड़ता है। घर के अन्दर बैठे रहने से काम नहीं चलता। घूमने-फिरने, दौरा करते रहने से यात्रा-भत्ता (टी.ए.) दैनिक-भत्ता (डी.ए.) आदि में कुछ रुपये बनते हैं। अधिकांश समय तो व्यस्तता ही अपनी बढ़ती हुई आयु की बात भी भुलाये रखती है। कभी-कभी घूमते-घूमते थक जाता हूँ। बस तभी, कभी-कभी मैं अनुभव करता हूँ, मैं उम्र के पचास वर्ष पार कर चुका हुआ एक बूढ़ा आदमी हूँ। मन्त्री होने से अभाव, कमी, दुःख, दरिद्र कम हो सकता है परन्तु वयस ? अर्थात आयु तो कम नहीं होती।
अध्यापकीय जीवन में शिक्षा दे-देकर पढ़ा-पढ़ाकर, जो धन अर्जित किया था, उसके सहारे निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन होता था। समय-समय पर बीच-बीच में उधार लेना पड़ता था। विद्यालय के अध्यापक उधार के रुपये बैंक से कर्ज नहीं लेते, उधार लेते हैं साथ के ही अन्य सहयोगी अध्यापक से। इनसे-उनसे (ये उनसे, वे इनसे) उधार लेकर खर्च चलाने में कोई लाज-संकोच नहीं करते। किसी-किसी दिन और कहीं तालमेल न बैठा सका तो मैं एक आदमी से उधार लेता हूँ, उसी तरह किसी-किसी दिन एक आदमी मुझसे उधार लेता है। जिस दिन वेतन मिलता है, उस दिन फिर सारा कुछ लेन-देन का हिसाब-किताब दुरुस्त कर लिया जाता है। कभी-कभी किश्त-किश्त करके, किश्तों में भी उधार लौटाने, निबटाने का इन्तजाम कर लिया करते हैं।
मेरे मन्त्री बन जाने के बाद से ही मेरे गाँव के लोगों ने मुझे अनेक बार गाँव में आमन्त्रित किया है। पहले मैं जिस कँहुवानी उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवा कार्य करता था, उस विद्यालय के छात्रों-अध्यापकों ने भी कई बार बुलाया है, मेरा अभिनन्दन करने के लिए। विद्यालय के आस-पास के गाँवों की साधारण प्रजा ने भी अपने गाँवों में सादर आमन्त्रित किया है। अत्यन्त व्यस्तता में, कार्यक्रम बैठा न पाने के कारण ही अभी तक उन लोगों के आमन्त्रण पर जा नहीं पाया।
आज भले ही मैं मन्त्री हो गया हूँ, तथापि, मैं अपने जीवन के आरम्भिक दिनों की बातें, अपने बचपन की बाते उठती किशोरावस्था, युवावस्था की बातें बराबर भुलाये हुए नहीं तो रह सकता अपने घर वाले गाँव से छह मील दूर पैदल चल-चलकर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल) में जाकर पढ़ाई की थी। सूरज की प्रखर धूप, भीषण गर्मी, मूसलाधार वर्षा किसी की भी परवाह किये बिना खेत में हल जोतकर खेती-बारी की थी। गाँव के संगी-साथी आदमियों के साथ दस मील दूर तक पैदल जाकर झील में मछलियाँ पकड़ा करता था। उस समय किये गये शारीरिक-श्रम में भी एक आनन्द था। थकान में भी एक तृप्ति थी। काम करने में जो देह को कष्ट होता था, उस कष्ट को कर गुजरने के बाद उभरी हुई चेतना मन में उत्साह और प्रेरणा जगाती थी। मगर अब तो ‘‘बूढ़े भैंसे को सींग ही महा भार’’ हो गयी है। इस समय मंत्री बन जाने के पश्चात यदि दो दिन का विश्राम लेना चाहें, तो चिकित्सालय (हास्पिटल) में रोगी के रूप में भर्ती होकर जनता से दूर भाग जाने के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। वहाँ भी रोगी का हाल-चाल पूछने, खोज-खबर लेने आये आदमियों की भारी भीड़ जुट जाती है।
तमाम सारी व्यस्तताओं में भी, जनता के प्रबल आग्रह पर एक कार्यक्रम निश्चित किया, एक दुपहरी का; अपने गाँव से पन्द्रह मील दूर स्थित कँहुवानी गाँव की राजकीय सभा में भाग लेने का। वहाँ पर, वहाँ की जनता ने मेरे सम्मान अभ्यर्थना में, आतिथ्य-अभिनन्दन में कोई बहुत बड़ा आयोजन न कर पाने पर भी अपनी सामर्थ्य भर श्रेष्ठ आयोजन किया है। वहाँ पर मेरे बहुत सारे इष्ट-मित्र और जान पहचान के अनेक लोग हैं। अपने गाँव में मुझे आमन्त्रित कर वे लोग कुछ राजकीय प्रसाद देंगे। जैसे-विद्यालय के भवन को बनवाने के लिए रुपये देने की जरूरत है। गाँव की मुख्य सड़क को पक्का करवाने की जरूरत है। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए एक नलकूप लगवाना चाहिए। नौजवान लड़कों के लिए एक संघ बनाने और खेल के मैदान के निर्माण के लिए रुपये दिये जाने चाहिए।...आदि-आदि।
असीमिया आदमी सामूहिक हित की बात सोचता है, कभी भी केवल अपने लाभ के विषय में नहीं सोचता। सोचता है स्थान के लिए, अपने अंचल, (क्षेत्र) के हित के लिए, साधारण जनता के हित के लिए। राजकीय सम्पत्ति ही जन-साधारण की सम्पत्ति है। गाँव का आदमी शहर में जाकर किसी विधायक या मन्त्री से अकेले में मिल पाने में सफल होने पर भी अपने निजी हित के काम की जगह-‘‘हमारे गाँव की उस सड़क के लिए कुछ करने की जरूरत है न ?’’ कह कर जनता के हित की बात ही कह आता है।
पहले मैं भी इसी प्रकार जनता का प्रतिनिधि बनकर मन्त्री आदि के पास पहुँचता था। इस समय अब जनता मेरे पास आती है।
कहुँवानी गाँव मेरा बहुत-पुरानी जान-पहचान का अच्छी तरह जाना-बूझा गाँव है। आस-पास के कई गाँवों की प्रजा ने मिलकर वहाँ पर अत्यन्त उत्साह से एक बहुत विशाल-सभा मण्डप बनाकर विशाल सभा का आयोजन किया है। क्योंकि एक मन्त्री तो हमेशा (बार-बार) गाँव-गाँव चक्कर नहीं लगा सकता।
कहुँवानी गाँव की बातें याद पड़ने पर रह-रहकर मुझे पुण्यकांत नाथ मास्टर की बातें याद हो आती हैं। मैं जब उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आया, उसके दो वर्ष बाद ही वे अपनी शिक्षक सेवा से सेवानिवृत्त हो गये थे। उस समय काम करते हुए-मैं अपनी ओर से, विद्यालय की ओर जाता था, और वे मेरी दूसरी ओर से, उस छोर से अपनी पुरानी साइकिल को चलाते हुए विद्यालय आते थे। साइकिल खराब हो जाने पर कभी-कभी पैदल ही चले आते थे। यद्यपि उनकी उम्र काफी हो गयी थी, तथापि उनका स्वास्थ्य अच्छा था। और विद्यालय आने के विषय में वे समयनिष्ठ (पंक्चुएल) तथा नियमित थे, जरा भी हेर-फेर नहीं होने देते थे।
समय के प्रति चूँकि वे इतने अधिक सजग और सचेत न थे, इसी वजह से विद्यालय के छात्रों ने उनका नाम ही रख दिया था-‘घड़ी मास्टर !’’ इसी तरह चूँकि मैं बराबर सभा-समितियों में भाग लेता फिरता रहता था अतः मेरा नाम रख दिया था-‘समिति-मास्टर’। नाथ मास्टर सदा एक पुरानी घड़ी अपनी जेब में लिए फिरते थे। एक ही विद्यालय में बिना किसी व्यवधान के, लगातार पैंतीस वर्षों तक शिक्षण सेवा कार्य करते हुए वे सेवा निवृत्त हुए थे। गणित और अंग्रेजी विषय के अति पारंगत विद्वान् थे, परन्तु चूँकि ग्रैजुएशन की डिग्री उनके पास नहीं थी, अतः विद्यालय की कुछ निचली कक्षाओं में ही पढ़ाया करते थे।
नाथ मास्टर का नाम ‘घड़ी मास्टर’ के रूप में विख्यात होने के सम्बन्ध में एक बात बहुत प्रचारित थी, वह सही थी कि गलत ? मैं इस सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक कुछ कह नहीं सकता। वह बात यह है कि- वे चाहे जहाँ कहीं रहें, पाँच मिनट या दस मिनट बाद घड़ी निकाल-निकालकर समय कितना हुआ देखते रहते थे। यहाँ तक कि साइकिल पर सवारी कर चलाते हुए जब आते रहे होते, तब भी। पोखरे या तालाब में जब स्नान करने के लिए जाते, तब भी घड़ी को साथ लिये जाते; और बाँस या लकड़ी के मचान या पुल पर, अथवा पोखरे के किनारे घड़ी को सम्भालकर रख लेने के बाद ही स्नान करते थे।
एक बार सरस्वती पूजा के उत्सव में नाथ मास्टर की वह घड़ी अचानक खो गयी। बहुत ढूँढ़ने-ढाढ़ने पर भी न मिली, तो नहीं ही मिली। ‘‘विद्यालय के ही किसी शरारती छात्र ने जान-बूझकर चुरा लिया है-’’ ऐसा एक निष्कर्ष-सा मान लिया गया। नाथ-मास्टर को बहुत हार्दिक सदमा-सा लगा, उनका मन मुरझा गया। घड़ी के अभाव में वे पल भर भी नहीं रह सकते थे। एक सप्ताह के अन्दर ही उन्होंने नाना तरह के उपाय कर एक सौ पचीस रुपये जुटा लिये और उन एक सौ पचीस रुपये से एक घड़ी, हाथ में बाँधी जाने वाली घड़ी (रिस्ट वाच), नयी घड़ी खरीद ली। अपने मासिक वेतन के साथ, पहले से बचाकर जुगाड़े गये रुपयों को भी मिला देने पर भी जब काम नहीं बन सका, तब उन्होंने कुछ अन्य अध्यापकों से भी कुछ रुपये उधार लिये थे, बीस रुपये या कि तीस रुपये या जाने कितने उधार लिये थे, मैं इस समय भूल गया हूँ। पहले वाली घड़ी के खो जाने से वे अतिशय उदास और खिन्न हो गये थे। अब हाथ में इस नयी घड़ी को पहनकर वे परम प्रफुल्लित हो गये। घड़ी के प्रति उनके इसी प्रकार के मोह और आसक्ति को लक्ष्य कर ही छात्र-छात्राओं ने उनका नाम ‘घड़ी मास्टर’ रख दिया था। उनकी अनुपस्थिति में हम लोग भी उन्हें इसी नाम से सम्बोधित करते थे। कुछ एक शरारती लड़कों ने उनकी घड़ी के सम्बन्ध में कुछ कहानियाँ भी गढ़कर प्रचारित कर दी थीं। जिनमें से दो इस प्रकार हैं :
‘‘नाथ-मास्टर हमेशा सबेरे खूब तड़के भोर में नींद से जग पड़ते हैं। और उठ बैठते ही सबसे पहले अपनी घड़ी में समय देखते हैं, उसके बाद पूरब में उगते सूर्य की ओर देखते हैं। तब कहते हैं-हाँ, आज सूर्य ठीक समय से उदय हुआ है। मेरी घड़ी के समय के साथ उसका समय ठीक-ठीक मिल रहा है। चार बजकर सत्ताईस मिनट पर आज सूर्य को उदित होना चाहिए।’’
सूर्य मानो ‘‘घड़ी मास्टर’’ की घड़ी के समय के मुताबिक ही उगता है।
एक दिन ऐसा हुआ कि सूर्य उग जाने के बाद लगभग सात बज चुके थे। परन्तु मास्टर कहते थे कि नहीं अभी सूर्य नहीं उगा है। इतनी जल्दी सूर्य उग ही नहीं सकता।
बाद में पता लगाया तो मालूम हुआ की घड़ी मास्टर की वह घड़ी रात ही से बन्द हो गयी है, अर्थात रात के तीन बजने के बाद से ही।’’
मुझ जैसे आदमी के एक प्रदेश का एक मन्त्री बन जाना, कभी-कभी मुझे स्वयं ही एक अविश्वसनीय घटना जान पड़ती है। पहले ही विधायक (एम.एल.ए.) या मन्त्री होना बहुत बड़ी बात जान पड़ती थी। और क्या कहें ? किसी को विधायक या मन्त्री बनवाने के लिए निर्वाचन के समय मतदान का मत (वोट) जुटाने के लिए दौड़-धूप करना भी, एक विशेषतापूर्ण, अति-महत्त्वपूर्ण बात जान पड़ती थी, किन्तु अब तो मैं स्वयं ही एक मन्त्री हूँ। गणतंत्र में सभी कुछ सम्भव है। अन्यथा, यदि ऐसा न होता तो, मुझ जैसे एक गँवईं-गँवार के उच्च-माध्यमिक विद्यालय (हाई-स्कूल) के एक सहायक अध्यापक के किसी दिन मन्त्री बन जाने की घटना एक अविश्वसनीय बात ही समझनी पड़ती।
हाँ, इतना जरूर है कि अध्यायन कार्य करते हुए मैं थोड़ी-थोड़ी राजनीति भी नहीं करता रहा, ऐसा भी नहीं। हमारे इस देश में दुःखी, दरिद्र व्यक्ति ही राजनीति अधिक करते हैं। जिन दिनों मैं विद्यालय में अध्यापन करता था, उन दिनों माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक भी इन्हीं दुःखी-दरिद्रों की श्रेणी में आते थे। उन दिनों हमारा विद्यालय एक दैनिक समाचार-पत्र, एक या कि दो साप्ताहिक, पाक्षिक पत्रिका मँगवाया करता था। वही सब अध्यापकों के सामूहिक-कक्ष (कॉमन-रूम) की सार्वजनिक सम्पत्ति थी। उन्हें सभी पढ़ते थे। उनमें प्रकाशित कुछ बातों को लेकर सभी आपस में आलोचना-प्रत्यालोचना करते थे। कभी-कभी उन्हीं में से वे किसी विशेष बात को लेकर, या समाचार को लेकर आपस में तर्कातर्कि, वाद-विवाद करने में मशगूल हो जाते, इसी प्रकार के तर्कातर्कि, वाद-विवाद का दूसरा नाम है राजनीति। इस प्रकार की तर्कातर्कि, आलोचना-प्रत्यालोचना में मैं भी भाग लेता था। और विद्यालय के बाहर होने वाली साधारण जन सभाओं, सभा-समितियों में भी प्रायः योगदान करता था। अतएव वही सब कुछ राजनीति था।
उसके बाद तो फिर सचमुच की राजनीति में प्रवेश कर गया। एक राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य के रूप में जो आरम्भ किया तो क्रमशः एक स्थानीय छोटे नेता के स्तर तक ऊँचा उठ गया। उसके बाद तो सभा-समितियों, समारोहों के लिए प्रायः एक अपरिहार्य नेता ही हो गया। इस तरह मेरी कार्य व्यस्तता और मेरी महिमा काफी बढ़ गयी।
फिर उसके पश्चात् अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाने पर विधायक (एम.एल.ए) के निर्वाचन में प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ। निर्वाचन का खेल खेलने के लिए मेरे राजनीतिक दल ने भी पर्याप्त मात्रा में रुपया प्रदान किया। निर्वाचन या चुनाव के खेल को खेल कहना तनिक भी असंगत नहीं है। दरअसल, यह भी एक खेल ही है। इसमें भी (खेल प्रतियोगिता की भाँति) पक्ष है, विपक्ष है, दलबन्दी है, हार-जीत है। इस खेल के भी अपने नियम- निर्देश हैं। खेल के कला-कौशल, नियम-कायदों से अनभिज्ञ होने पर हार जाना ही स्वाभाविक है। हाँ, अन्य खेलों में साधारणतः दो दल या टीमें होती हैं, परन्तु निर्वाचन या चुनाव में यदा-कदा ही, कभी-कभार ही मात्र दो दल होते हैं। प्रायः कई-कई दल इस एक ही खेल को खेलने के लिए खेल-मैदान में उतरते हैं। पैरों से खेलने की गेंद, फुटबाल, गेंद और बल्ले का खेल, क्रिकेट, हाकी आदि खेलों में विजयश्री पाना या जीत प्राप्त करना निर्भर करता है खेलने वाले खिलाड़ी की कला-दक्षता पर। परन्तु हमारे देश, में निर्वाचन या चुनाव के इस खेल में विजयश्री या जीत प्रत्याशी के गुण-अवगुण पर निर्भर नहीं होती। मुख्य रूप से वह निर्भर करती है, रुपये पर। इसे देखकर ही निर्वाचन या चुनाव के इस खेल को बहुत से लोग ‘रुपये का खेल’ कहकर ही पुकारते हैं। दुःखी-दरिद्र, गरीब लोगों से भरे एक देश में भले ही ऐसी बात कहने का सुयोग नहीं है। परन्तु और कोई व्यक्ति इस बात को यदि स्वीकार न भी करे तो अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों से, अपने स्वयं भोगे हुए अनुभवों से मैं यह कह सकता हूँ कि इस बात में बहुलांश में, अधिकाधिक मात्रा में सच्चाई है। रुपया न होने से निर्वाचन या चुनाव नहीं होता। रुपया न होने पर हम विधायक (एम.एल.ए.), मन्त्री कुछ भी नहीं बन सकते।
मैंने भी निर्वाचन में क्या कोई कम रुपये खर्च किये ? हाँ, यह सच है कि खर्च करने के लिए मेरे पास अपना निजी संग्रहीत रुपया नहीं था। अध्यापकी कर-करके जो रुपये पा सका था, उससे तो महीना बिता पाना ही कठिन था। (घर के अत्यावश्यक खर्चों के लिए ही वह महीने भर को नहीं पोसाता था) इस तरह जो कुछ रुपये मैं कमा सका था, उसके हिसाब से एक निर्वाचन चुनाव लड़ने में खर्च होने वाले रुपये तो मैं तीन जन्मों में भी नहीं कमा सकता था। मेरे निर्वाचन में खर्च करने के लिए इतने अधिक रुपये कहाँ से, किस विधि से आये, यह एक खुली हुई अतिगोपनीय कहानी है।
निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए दल के प्रत्याशी चुन लिये जाने के बाद कुछ रुपये मैंने किसी-किसी से उधार में भी लिये थे। उस समय जिस किसी के पास भी रुपये थे, उनमें से किसी ने भी रुपये उधार देने से इनकार नहीं किया था। कुछ लोग तो ऐसे भी थे, जिनके पास यदि खुद का पैसा नहीं था, तो उन्होंने दूसरों से उधार लेकर मुझे रुपये दिये। मेरे अपने परिवार और नाते-रिश्ते के लोगों के अतिरिक्त मेरे विद्यालय के सहकर्मी सारे अध्यापकों ने भी अपनी-अपनी औकात के मुताबिक मुझे रुपये देकर मेरी सहायता की। और-तो-और यहाँ तक कि एक ही विद्यालय में पढ़ाने का काम करके जो अध्यापक सेवा-निवृत्त हो चुके थे उनमें से भी दो एक जनों ने मुझे रुपये दिये थे। जो स्वयं नहीं आ सकते थे, उन्होंने किसी और के हाथों रुपये भिजवा दिये थे।
रुपये देकर इसी प्रकार से सहायता प्रदान करने वाले सेवा निवृत्त एक अध्यापक थे श्री पुण्यकान्त नाथ। कुछ वर्षों पहले ही वे सेवा निवृत्त हुए थे। उन्होंने एक आदमी के हाथों मेरे निर्वाचन खर्च के लिए बीस रुपये पठवाये थे, उसी के साथ मेरी विजय के लिए शुभकामना प्रकट करते हुए एक छोटा-सा पत्र भी भेजा था-
‘‘तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ जिससे कि तुम्हारी विजय हो। विजयी होकर जनता की भलाई करोगे, ऐसी आशा रखता हूँ। यदि मेरे पास होता तो बढ़ाकर दो रुपये और पठाए होता। मेरी अवस्था तो जानते ही हो। आशा करता हूँ बुरा नहीं मानोगे।–पुण्यकान्त।’’
बहुत सम्भव है सभी लोगों के आशीर्वाद और शुभ-कामनाओं के भरोसे मैं निर्वाचन में विजयी हुआ (विधायक चुना गया) और सरकार में मन्त्री भी बन गया।
मन्त्री बन जाने के बाद धीरे-धीरे मैंने अनेक लोगों को उनके द्वारा दिये गये उधार, उनके रुपये वापस लौटा दिये। किसी-किसी ने उसे वापस लिया, अधिकांश ने नहीं लिया। उसके बदले में उन्होंने अपना कोई-कोई, यह या वह, काम करवा लिया। किसी के लिए नौकरी, किसी का तबादला, किसी को पदोन्नति, किसी के लिए लाइसेन्स, परमिट आदि मंजूर करवा लिया।
प्रायः सभी ने प्रसन्न मन से हँस-हँस कर कहा-‘‘अरे रुपये की भी कोई बात है ? हमारा रुपया जो व्यर्थ नहीं हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। इस तरह मेरे निर्वाचन की वेला में रुपये उधार देकर, बाद में मेरे द्वारा लौटाये जाने पर भी जिन महान व्यक्तियों ने उसे वापस नहीं लिया, उन लोगों को मैंने हृदय से अपना अत्यन्त उपकारकर्त्ता और शुभचिन्तक माना। ‘‘मछली चाहिए या कि झील चाहिए ?’’ इस तरह की लोकोक्तिपरक पिपासा पर वे सभी लोग झील लेने के पक्ष में थे। क्योंकि झील के अपने कब्जे में बने रहने पर आखिर मछली कहाँ भाग कर बचेगी ?’’
मन-ही-मन मैंने अत्यन्त हार्दिक आनन्द का अनुभव किया। (यह सब मुझे बहुत अच्छा लगा) निर्वाचन की लड़ाई जीतने के लिए जो तमाम सारे रुपये मैंने पाये थे, यदि वह सारा-का-सारा फिर से लौटा देना पड़ता, तो मन्त्री के रूप में जो रुपये कमा रहा था, उसमें से कई महीनों की कमाई का रुपया खर्च कर देने को मजबूर हो गया होता। और यदि सचमुच ही ऐसा कर देना पड़ा होता तो इतने कम समय के अन्दर राजधानी में मकान बनाने के लिए जमीन नहीं खरीद पाये होता, और उस पर यह तीन मंजिला भवन भी नहीं गढ़वा पाये होता, यहाँ तक कि नयी कार खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपना नाम भी रजिस्टर नहीं करवा सका होता।
मन्त्री को जन-साधारण में ख्याति प्राप्त करने के लिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए जनता के बीच घूमना-फिरना पड़ता है, दौड़-धूप करनी होती है। सभा-समितियों में भाग लेना, सभा-समितियों का आयोजन करना पड़ता है। घर के अन्दर बैठे रहने से काम नहीं चलता। घूमने-फिरने, दौरा करते रहने से यात्रा-भत्ता (टी.ए.) दैनिक-भत्ता (डी.ए.) आदि में कुछ रुपये बनते हैं। अधिकांश समय तो व्यस्तता ही अपनी बढ़ती हुई आयु की बात भी भुलाये रखती है। कभी-कभी घूमते-घूमते थक जाता हूँ। बस तभी, कभी-कभी मैं अनुभव करता हूँ, मैं उम्र के पचास वर्ष पार कर चुका हुआ एक बूढ़ा आदमी हूँ। मन्त्री होने से अभाव, कमी, दुःख, दरिद्र कम हो सकता है परन्तु वयस ? अर्थात आयु तो कम नहीं होती।
अध्यापकीय जीवन में शिक्षा दे-देकर पढ़ा-पढ़ाकर, जो धन अर्जित किया था, उसके सहारे निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन होता था। समय-समय पर बीच-बीच में उधार लेना पड़ता था। विद्यालय के अध्यापक उधार के रुपये बैंक से कर्ज नहीं लेते, उधार लेते हैं साथ के ही अन्य सहयोगी अध्यापक से। इनसे-उनसे (ये उनसे, वे इनसे) उधार लेकर खर्च चलाने में कोई लाज-संकोच नहीं करते। किसी-किसी दिन और कहीं तालमेल न बैठा सका तो मैं एक आदमी से उधार लेता हूँ, उसी तरह किसी-किसी दिन एक आदमी मुझसे उधार लेता है। जिस दिन वेतन मिलता है, उस दिन फिर सारा कुछ लेन-देन का हिसाब-किताब दुरुस्त कर लिया जाता है। कभी-कभी किश्त-किश्त करके, किश्तों में भी उधार लौटाने, निबटाने का इन्तजाम कर लिया करते हैं।
मेरे मन्त्री बन जाने के बाद से ही मेरे गाँव के लोगों ने मुझे अनेक बार गाँव में आमन्त्रित किया है। पहले मैं जिस कँहुवानी उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवा कार्य करता था, उस विद्यालय के छात्रों-अध्यापकों ने भी कई बार बुलाया है, मेरा अभिनन्दन करने के लिए। विद्यालय के आस-पास के गाँवों की साधारण प्रजा ने भी अपने गाँवों में सादर आमन्त्रित किया है। अत्यन्त व्यस्तता में, कार्यक्रम बैठा न पाने के कारण ही अभी तक उन लोगों के आमन्त्रण पर जा नहीं पाया।
आज भले ही मैं मन्त्री हो गया हूँ, तथापि, मैं अपने जीवन के आरम्भिक दिनों की बातें, अपने बचपन की बाते उठती किशोरावस्था, युवावस्था की बातें बराबर भुलाये हुए नहीं तो रह सकता अपने घर वाले गाँव से छह मील दूर पैदल चल-चलकर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल) में जाकर पढ़ाई की थी। सूरज की प्रखर धूप, भीषण गर्मी, मूसलाधार वर्षा किसी की भी परवाह किये बिना खेत में हल जोतकर खेती-बारी की थी। गाँव के संगी-साथी आदमियों के साथ दस मील दूर तक पैदल जाकर झील में मछलियाँ पकड़ा करता था। उस समय किये गये शारीरिक-श्रम में भी एक आनन्द था। थकान में भी एक तृप्ति थी। काम करने में जो देह को कष्ट होता था, उस कष्ट को कर गुजरने के बाद उभरी हुई चेतना मन में उत्साह और प्रेरणा जगाती थी। मगर अब तो ‘‘बूढ़े भैंसे को सींग ही महा भार’’ हो गयी है। इस समय मंत्री बन जाने के पश्चात यदि दो दिन का विश्राम लेना चाहें, तो चिकित्सालय (हास्पिटल) में रोगी के रूप में भर्ती होकर जनता से दूर भाग जाने के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। वहाँ भी रोगी का हाल-चाल पूछने, खोज-खबर लेने आये आदमियों की भारी भीड़ जुट जाती है।
तमाम सारी व्यस्तताओं में भी, जनता के प्रबल आग्रह पर एक कार्यक्रम निश्चित किया, एक दुपहरी का; अपने गाँव से पन्द्रह मील दूर स्थित कँहुवानी गाँव की राजकीय सभा में भाग लेने का। वहाँ पर, वहाँ की जनता ने मेरे सम्मान अभ्यर्थना में, आतिथ्य-अभिनन्दन में कोई बहुत बड़ा आयोजन न कर पाने पर भी अपनी सामर्थ्य भर श्रेष्ठ आयोजन किया है। वहाँ पर मेरे बहुत सारे इष्ट-मित्र और जान पहचान के अनेक लोग हैं। अपने गाँव में मुझे आमन्त्रित कर वे लोग कुछ राजकीय प्रसाद देंगे। जैसे-विद्यालय के भवन को बनवाने के लिए रुपये देने की जरूरत है। गाँव की मुख्य सड़क को पक्का करवाने की जरूरत है। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए एक नलकूप लगवाना चाहिए। नौजवान लड़कों के लिए एक संघ बनाने और खेल के मैदान के निर्माण के लिए रुपये दिये जाने चाहिए।...आदि-आदि।
असीमिया आदमी सामूहिक हित की बात सोचता है, कभी भी केवल अपने लाभ के विषय में नहीं सोचता। सोचता है स्थान के लिए, अपने अंचल, (क्षेत्र) के हित के लिए, साधारण जनता के हित के लिए। राजकीय सम्पत्ति ही जन-साधारण की सम्पत्ति है। गाँव का आदमी शहर में जाकर किसी विधायक या मन्त्री से अकेले में मिल पाने में सफल होने पर भी अपने निजी हित के काम की जगह-‘‘हमारे गाँव की उस सड़क के लिए कुछ करने की जरूरत है न ?’’ कह कर जनता के हित की बात ही कह आता है।
पहले मैं भी इसी प्रकार जनता का प्रतिनिधि बनकर मन्त्री आदि के पास पहुँचता था। इस समय अब जनता मेरे पास आती है।
कहुँवानी गाँव मेरा बहुत-पुरानी जान-पहचान का अच्छी तरह जाना-बूझा गाँव है। आस-पास के कई गाँवों की प्रजा ने मिलकर वहाँ पर अत्यन्त उत्साह से एक बहुत विशाल-सभा मण्डप बनाकर विशाल सभा का आयोजन किया है। क्योंकि एक मन्त्री तो हमेशा (बार-बार) गाँव-गाँव चक्कर नहीं लगा सकता।
कहुँवानी गाँव की बातें याद पड़ने पर रह-रहकर मुझे पुण्यकांत नाथ मास्टर की बातें याद हो आती हैं। मैं जब उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आया, उसके दो वर्ष बाद ही वे अपनी शिक्षक सेवा से सेवानिवृत्त हो गये थे। उस समय काम करते हुए-मैं अपनी ओर से, विद्यालय की ओर जाता था, और वे मेरी दूसरी ओर से, उस छोर से अपनी पुरानी साइकिल को चलाते हुए विद्यालय आते थे। साइकिल खराब हो जाने पर कभी-कभी पैदल ही चले आते थे। यद्यपि उनकी उम्र काफी हो गयी थी, तथापि उनका स्वास्थ्य अच्छा था। और विद्यालय आने के विषय में वे समयनिष्ठ (पंक्चुएल) तथा नियमित थे, जरा भी हेर-फेर नहीं होने देते थे।
समय के प्रति चूँकि वे इतने अधिक सजग और सचेत न थे, इसी वजह से विद्यालय के छात्रों ने उनका नाम ही रख दिया था-‘घड़ी मास्टर !’’ इसी तरह चूँकि मैं बराबर सभा-समितियों में भाग लेता फिरता रहता था अतः मेरा नाम रख दिया था-‘समिति-मास्टर’। नाथ मास्टर सदा एक पुरानी घड़ी अपनी जेब में लिए फिरते थे। एक ही विद्यालय में बिना किसी व्यवधान के, लगातार पैंतीस वर्षों तक शिक्षण सेवा कार्य करते हुए वे सेवा निवृत्त हुए थे। गणित और अंग्रेजी विषय के अति पारंगत विद्वान् थे, परन्तु चूँकि ग्रैजुएशन की डिग्री उनके पास नहीं थी, अतः विद्यालय की कुछ निचली कक्षाओं में ही पढ़ाया करते थे।
नाथ मास्टर का नाम ‘घड़ी मास्टर’ के रूप में विख्यात होने के सम्बन्ध में एक बात बहुत प्रचारित थी, वह सही थी कि गलत ? मैं इस सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक कुछ कह नहीं सकता। वह बात यह है कि- वे चाहे जहाँ कहीं रहें, पाँच मिनट या दस मिनट बाद घड़ी निकाल-निकालकर समय कितना हुआ देखते रहते थे। यहाँ तक कि साइकिल पर सवारी कर चलाते हुए जब आते रहे होते, तब भी। पोखरे या तालाब में जब स्नान करने के लिए जाते, तब भी घड़ी को साथ लिये जाते; और बाँस या लकड़ी के मचान या पुल पर, अथवा पोखरे के किनारे घड़ी को सम्भालकर रख लेने के बाद ही स्नान करते थे।
एक बार सरस्वती पूजा के उत्सव में नाथ मास्टर की वह घड़ी अचानक खो गयी। बहुत ढूँढ़ने-ढाढ़ने पर भी न मिली, तो नहीं ही मिली। ‘‘विद्यालय के ही किसी शरारती छात्र ने जान-बूझकर चुरा लिया है-’’ ऐसा एक निष्कर्ष-सा मान लिया गया। नाथ-मास्टर को बहुत हार्दिक सदमा-सा लगा, उनका मन मुरझा गया। घड़ी के अभाव में वे पल भर भी नहीं रह सकते थे। एक सप्ताह के अन्दर ही उन्होंने नाना तरह के उपाय कर एक सौ पचीस रुपये जुटा लिये और उन एक सौ पचीस रुपये से एक घड़ी, हाथ में बाँधी जाने वाली घड़ी (रिस्ट वाच), नयी घड़ी खरीद ली। अपने मासिक वेतन के साथ, पहले से बचाकर जुगाड़े गये रुपयों को भी मिला देने पर भी जब काम नहीं बन सका, तब उन्होंने कुछ अन्य अध्यापकों से भी कुछ रुपये उधार लिये थे, बीस रुपये या कि तीस रुपये या जाने कितने उधार लिये थे, मैं इस समय भूल गया हूँ। पहले वाली घड़ी के खो जाने से वे अतिशय उदास और खिन्न हो गये थे। अब हाथ में इस नयी घड़ी को पहनकर वे परम प्रफुल्लित हो गये। घड़ी के प्रति उनके इसी प्रकार के मोह और आसक्ति को लक्ष्य कर ही छात्र-छात्राओं ने उनका नाम ‘घड़ी मास्टर’ रख दिया था। उनकी अनुपस्थिति में हम लोग भी उन्हें इसी नाम से सम्बोधित करते थे। कुछ एक शरारती लड़कों ने उनकी घड़ी के सम्बन्ध में कुछ कहानियाँ भी गढ़कर प्रचारित कर दी थीं। जिनमें से दो इस प्रकार हैं :
‘‘नाथ-मास्टर हमेशा सबेरे खूब तड़के भोर में नींद से जग पड़ते हैं। और उठ बैठते ही सबसे पहले अपनी घड़ी में समय देखते हैं, उसके बाद पूरब में उगते सूर्य की ओर देखते हैं। तब कहते हैं-हाँ, आज सूर्य ठीक समय से उदय हुआ है। मेरी घड़ी के समय के साथ उसका समय ठीक-ठीक मिल रहा है। चार बजकर सत्ताईस मिनट पर आज सूर्य को उदित होना चाहिए।’’
सूर्य मानो ‘‘घड़ी मास्टर’’ की घड़ी के समय के मुताबिक ही उगता है।
एक दिन ऐसा हुआ कि सूर्य उग जाने के बाद लगभग सात बज चुके थे। परन्तु मास्टर कहते थे कि नहीं अभी सूर्य नहीं उगा है। इतनी जल्दी सूर्य उग ही नहीं सकता।
बाद में पता लगाया तो मालूम हुआ की घड़ी मास्टर की वह घड़ी रात ही से बन्द हो गयी है, अर्थात रात के तीन बजने के बाद से ही।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i