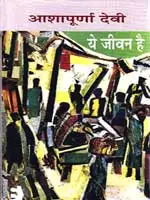|
कहानी संग्रह >> ये जीवन है ये जीवन हैआशापूर्णा देवी
|
372 पाठक हैं |
|||||||
इन कहानियों में मानव की क्षुद्र और वृहत् सत्ता का संघर्ष है, समाज की खोखली रीतियों का पर्दाफाश है और आधुनिक युग की नारी-स्वाधीनता के परिणामस्वरूप अधिकारों को लेकर उभर रहे नारी-पुरुष के द्वन्द्व पर दृष्टिपात है।
चरित्रहीन
अभी तक? इस उम्र में? सुनकर हैरान रह गया।
क्या सचमुच मनुष्य की वासना का अन्त नहीं है? असंयम की सीमा नहीं? क्या चरित्रहीन व्यक्ति इतना निर्लज्ज हो जाता है? मन-ही-मन उम्र का एक मोटा हिसाब लगाकर मैंने पाया कि वीरू मामा की उम्र लगभग सत्तर के करीब है। वही वीरू मामा अभी तक! आश्चर्य की बात है!
विदेश में रहता हूँ, कभी-कभार कोलकाता आता हूँ, वह भी छोटी-मोटी छुट्टियों में। नजदीकी रिश्तेदारों के कुशल समाचार लेने का ही समय नहीं बच पाता, तो ममेरे, चचेरे का क्या कहना! वीरू मामा अब तक जिन्दा हैं और इस धरती का अन्न फाँके जा रहे हैं इतना भी तो मालूम नहीं था, और समाचार तो दूर की बात। वीरू मामा के बेटे नीतू भैया आज मेरी माँ के पास अपना दुखड़ा रोने आये, तभी पता चला और जानकर हैरान रह गया। सोचा, चरित्रहीन हो जाने से क्या इतना निर्लज्ज हो जाता है आदमी?
बचपन से सुनता आया हूँ ज़रूर कि वीरू मामा का चरित्र ठीक नहीं, बीवी-बच्चों के होते हुए भी एक और उपसर्ग है, इत्यादि।
और वह उपसर्ग भी और कहीं की नहीं, अपने गाँव की ही है। आँधी-पानी, वज्रपात हो, दुनिया ही उलट जाए, तो भी प्रति रविवार को वीरू मामा गाँव जाते ही हैं, वह आकर्षण जन्मभूमि का नहीं, बुआ-चाचा का भी नहीं, उसी 'बेशर्म औरत' का है।
तब हम बच्चे थे इस कारण हमारे कान बचाकर बातें की जाती थीं, ऐसा याद नहीं आता। इसलिए तभी हमें पता चल गया था वीरू मामा बुरे आदमी हैं।
मगर वह आज की बात थोड़े ही है?
इतने बरसों बाद फिर वही बात कानों में आयी कि वीरू मामा उस बेशर्म औरत से...नहीं, अब इस बुढ़ापे में हफ्ते-हफ्ते गाँव जाने का कष्ट सहन नहीं होता, इसलिए गाँव के मकान में ही बस गये हैं वीरू मामा। बेटे उन्हें कोलकाता लाने के लिए मिन्नतें किये जा रहे हैं, मगर टस से मस नहीं हो रहे हैं वे।
उनके बहानों की भी कोई कमी नहीं है।
दिमाग बिलकुल साफ है।
बहाना यही लगाते हैं कि इस बुढ़ापे में कोलकाता के किराये के घर में भेड़िया-धसान होकर रहने को तैयार नहीं हैं वे। उद्दण्ड, शरारती पोते-पोतियों का शोर-शराबा, रात-दिन भाभी के झगड़े, किचकिच से भी नफरत है उन्हें।
इसके अतिरिक्त उन्होंने बेटों से पूछा भी है, ला सकोगे वह सब कुछ जो मेरी सेहत ठीक रखने के लिए ज़रूरी है?
क्या जवाब देंगे उनके बेटे?
हामी भरें तो किस भरोसे पर? उम्र बढ़ गयी है, इस कारण स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन्हें बहुत चीज़ों की जरूरत होती है। उन्हें चाहिए प्रतिदिन एक सेर शुद्ध दूध, भात के साथ प्रतिदिन छटाँक-भर गाय के दूध की मलाई से निकाला हुआ शुद्ध घी, दोनों समय खेत से ताज़ा निकाली गयी शाक-सब्जी, ताजा चारा मछली की रसेदार तरकारी और चटनी। इसके ऊपर से और जितना भी हो, यह तो आवश्यक ही है। इसी तरह नियम से रहेंगे तो और पन्द्रह-बीस साल हँस-खेलकर जी लेंगे, ऐसा ही सोचते हैं वीरू मामा।
और, जीना भी चाहते हैं वे।
पैसे फेंकने से भी कोलकाता में ये सब मिल सकता है क्या। हालाँकि गाँव में भी अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ तो है। बहुत न सही, थोड़ा बहुत मिल ही जाता है कोशिश करने से।
मगर वह कोशिश करे कौन?
''और कौन।'' नीतू भैया नाराजगी दिखाकर बोले, ''बस वही। हम लोगों ने तो एक तरह से जाना ही छोड़ दिया है। बस, माहवार खर्चे का रुपया और जो उनकी फरमाइश रहती है, लेकर महीने में एक बार...''
''पैसे क्यों नहीं बन्द कर देता?'' मेरी माँ वीरांगना जैसे विक्रम के साथ बोल पड़ीं, ''फिर कैसे चुपचाप वापस नहीं लौटते, मैं भी देखतीं?''
निराश भाव से नीतू भैया बोले, ''यह कैसे हो सकता है?
''हो क्यों नहीं सकता है?'' माँ फिर से प्रोत्साहित होकर बोलीं, ''कहेगा, हम साधारण लोग हैं, हर महीने नकद रुपये निकालकर कहाँ से देंगे। साथ मिलकर रहो, खाओ-पिओ, बस।''
''फिर तो तुम ही लोग कहोगे कैसे कुलांगार बेटे हैं। बूढ़े बाप को खाना तक नहीं देते।''
''कोई नहीं कहेगा।'' फिर अपने आप बोल पड़ी माँ, ''बाप जब बाप जैसा हो तो बेटे सर पर बिठाकर रखेंगे। बाप बेइज्जती के काम करे तो कोई क्या इज्जत करेगा?''
नीतू भैया उदास होकर बोले, ''यह कौन समझेगा? बल्कि सभी समझेंगे, बहुएँ अपने बूढ़े ससुर के झमेले उठाना नहीं चाहती हैं, तभी बेटों ने बाप को वनवास दे दिया। उस पर से पैसे बन्द करना।''
''मगर इतना बढ़ गया कब?'' माँ बोलीं, ''यह बीमारी थी, बराबर ही मालूम था। सुशीला दीदी तो गाँव के रिश्ते में हमारी बहन लगती हैं, देखती रहीं बराबर। लोग हँसी-तमाशा भी करते थे, मगर इतनी बेशर्मी तो नहीं थी। वीरू भैया हर रविवार गाँव जाते, भेंट मुलाकात, बातचीत करते थे, इतना ही। हाँ, मगर हर महीने सुशीला दीदी को खर्चा दिया करते थे।''
थोड़े कौतूहल के साथ मैंने पूछा, ''अच्छा, उन दिनों तुम्हारे गाँव का समाज यह सब चलने देता था? सुशीलादी के माता-पिता नाराज़ नहीं होते थे?
''माँ-बाप गये भाड़ में। होश सँभालने के पहले ही सब खोकर चाचा-चाची के परिवार में भर्ती हो गयी। बचपन में तो चाची रोज़ ताने देकर कहा करती थी, ''काम की न काज की, सौ मन अनाज की। नहीं मिलेगा खाना!'' छोटा-सा मुँह लेकर लोगों के दरवाजे पर खड़ी होती थी। तरस खाकर लोग मुट्ठी भर खाने को दे देते थे। सभी तो कहीं-न-कहीं से रिश्ते के ही लगते थे।''
''और ससुराल?''
''वहाँ भी यही हाल। जैसा फूटा नसीब। एक लड़का देखकर चाचा-चाची ने ब्याह कर विदा तो कर दिया था। छ: महीने में ही उसे खत्म कर फिर चाचा के सर पर सवार हो गयी। उन्हें भी क्यों पसन्द हो? रोज खिट-पिट चलती। उसी सिलसिले में वीरू मामा का दिल पिघल गया। बोले, ''केवल एक मुट्ठी भात के लिए इतना लांछन। मैं दूँगा सुशीला के खाने का खर्चा।'' तब अच्छा कमा लेता था। मर्चेंट ऑफिस में बड़ा बाबू था, दया दिखाने की क्षमता भी रखता था। बस वही दया दिखाना ही आफत बन गया। सुशीलादी एकदम पिघल गयी, मेल-जोल बढ़ गया। चाचा ने विधवा लड़की के रीत-चरित्र देखकर धक्के देकर घर से निकाल दिया एक दिन। सुनी हुई बात है यह सब, ठीक से याद नहीं। मगर हम लोगों ने सुशीलादी को अपने बाप की टूटी झोंपड़ी में रहते, वीरू मामा के पैसे से अपना पेट पालते और गाँव-भर के लिए काम करते देखा है। तगड़ी जान है, जिसे ज़रूरत पड़ी वही पुकारता-सुशीला। मगर इस बात में इतनी लापरवाह...'' नीतू भैया बीच में टोक कर बोले, ''इतना बढ़ गया माँ की मौत के बाद। माँ चल बसी, बाबूजी की भी नौकरी चली गयी।''
''नौकरी चली गयी?''
''हाँ, ऑफिस में नया फ़ैशन हुआ, बूढ़ों को निकालो। जबकि उस साठ वर्ष की उम्र में भी दो जवान आदमी के बराबर मेहनत कर सकते थे वह। खैर, नौकरी तो गयी। और जाते ही उन्होंने कहना शुरू किर दिया, 'दफ्तर जाता था दिन-भर, एक तरह से दिन कट जाता था, अब इतनी कशमकश भीड़ में नहीं रह पाऊँगा।''
हम लोगों ने सोचा, बुरा ही क्या है। बहुएँ तो दिन-रात 'बाबूजी ने यह कहा, बाबूजी ने वह कहा' कहकर बखेड़ा खड़ा करती रहती हैं। गाँव में रह जाएँगे तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा। चारों भाई पन्द्रह रुपये के हिसाब से देंगे, अपना खाना वह खुद पका लेंगे, पुराने नौकर का बेटा काम-काज कर देगा, यही व्यवस्था की गयी। बाबूजी को भी बड़ा-उत्साह, बड़ा जोश आया। तब हमें क्या पता ये सब बेशर्मी होगी। अगले महीने ही जाकर देखा, चौके में सुशीला बुआ। जरा सोचिए, देखकर मन की क्या दशा हुई होगी। यह सब बराबर से मालूम तो था, पर एकदम इस तरह खुलकर। सफाई दी गयी-'इन्हें भी स्वयं पकाकर खाने में तकलीफ़ हो रही थी, उनका भी घर टूटकर गिर गया था, रहने की तकलीफ़ हो रही थी, इसीलिए।'' माँ उग्र स्वर में बोल उठीं, ''तुम लोगों ने कहा नहीं कुछ भी?''
''क्या कहें, बताइए? उन्हें शर्म न हो, हमें तो है। जैसे कुछ पता नहीं चला, ऐसा बहाना कर लौट आये। अब भी जाते हैं, एक शाम रहकर, खाना खाकर लौट आते हैं। मगर देखिए, इस महँगाई के ज़माने में घर से साठ रुपये निकल जाना। कोलकाता आकर रहते तो...''
मैं समझ गया नीतू भैया के कष्ट का मूल क्या है।
इसके बाद नीतू भैया और माँ के बीच जोरदार आलोचना शुरू हुई, किस तरह इस अवैध काण्ड को जड़ से निर्मूल किया जाय। ऐसा तय हुआ कि माँ एक बार स्वयं मुआयना करने जाएँगी और सारी मुसीबत की जड़ को खरी-खोटी सुनाकर, वीरू मामा को धिक्कार देकर यह बात समझाकर छोड़ेंगी कि समाज में रहकर यह सब असामाजिक बात नहीं चलेगी। कहेंगी कि इस पाप को विदा न कर दे तो बेटे माहवार का खर्चा देना बन्दकर देंगे। क्यों नहीं करेंगे भला? तुम बाप होकर अगर समाज में उन्हें मुँह दिखाने का रास्ता बन्द कर दो, तो अगर वे पैसे बन्द कर दें तो इसमें अपराध कैसा?
मैंने कहा, ''तुम क्यों दूसरों के मामले में टाँग अड़ाती हो माँ? जिसकी जो मर्जी कर रहा है, तुम्हें क्या पड़ी है?''
माँ ने धिक्कार देकर मुझे चुपकर दिया। बोली, ''तू कहता क्या है? मुझे क्या पड़ी है? वह घर मेरे बाप-दादा का नहीं है? वहाँ बैठकर जिसकी जो मर्जी, कर ले? मर्द है, बाहर जो करना हो कर ले, मगर घर में दुष्कर्म करेगा?''
शर्म-लिहाज़ छोड़कर मैं बोला, ''दुष्कर्म और क्या। उम्र का तो कोई हिसाब ही नहीं लगता।''
माँ झुकीं नहीं। बोलीं, ''तू चुपकर बोलू, उन्हें उम्र का ख्याल है क्या? अभी तक जितना लट-पट है...खैर, तेरे सामने अब क्या मुँह खोलूँ। सीधी बात यह है कि मैं वीरू भैया को जाकर समझा दूँगी कि बाप-दादा के घर बैठकर यह सब अनाचार नहीं चलेगा। शर्म-हया नहीं है क्या? अपने बच्चों के आगे सर उठाकर देखने का डर नहीं है क्या? झाड़ू मारती हूँ ऐसी प्रवृत्ति को।''
अन्त में मेरे ही ऊपर सवार होकर माँ ने बारूईपुर की यात्रा की। नीतू भैया नहीं जाएँगे, ऐसे में बच्चों का सामना नहीं होना ही अच्छा रहेगा।
किया ही क्या जाय?
मगर सच कहूँ तो जाने को इतना विमुख तो नहीं था, मुझे भी कौतूहल हो रहा था सत्तर वर्ष के उस प्रेमिक पुरुष को देखने का।
देखा भी।
और देखकर पहले ऐसा ही लगा, क्या सचमुच चरित्रहीन हो जाने से आदमी इतना बेशर्म हो जाता है?
सुदीर्घ तेजदीप्त चेहरा, आँखों में प्रसन्नता की झलक।
लज्जा, संकोच, दुविधा, इन चीज़ों का लेशमात्र नहीं। एकदम मुक्त पुरुष जैसे लगे। माँ को देखकर 'यंगमैन' की तरह चहचहा उठे, ''अरे कौन है रे! बुलबुलि है न? बात क्या है? तू कहाँ से? कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। बाप-दादा का घर याद है अभी तक? कोई नहीं आता है। जानती है बुलबुलि, कोई अब गाँव नहीं आता है। गाँव में अँधेरा छाया है।''
माँ तो इसी मौके पर कह सकती थीं, ''क्यों। तुम जो छाये हो गाँव-परिवार-वंश सब पर उजाला बनकर।'' नहीं तो यह भी कह सकती थीं, ''कोई आये भी तो किस खुशी में?''
''तुम्हारे जैसे कुल-तिलक जहाँ बस रहे हों, वहाँ कौन आये?''
कह पातीं तो बात आगे बढ़ जाती। मगर कहा नहीं। पता नहीं कहा नहीं या कह नहीं पायीं। बड़े दिनों का भूला हुआ 'बुलबुलि' नाम कानों के भीतर जाकर शायद स्वर में आवेग भर गया। बस देखने को इतना मिला कि माँ ने झुककर पूरे क़ायदे से ही प्रणाम किया वीरू मामा को।
तब तक एक बार फिर वीरू मामा शोर मचा उठे, ''अरे सुशीला, क्या फालतू के काम लेकर चौके में बैठी है? आकर देख तो सही, कौन आया है! बुलबुलि! हमारे मँझले चाचा की बेटी बुलबुलि। कैसी अच्छी-भली गृहिणी बन गयी है। यही तेरा बड़ा बेटा है न? कितना छोटा-सा देखा था इसे। करता क्या है रे?''
जवाब की अपेक्षा किये बिना ही प्रश्न पूछते गये वीरू मामा, और एकदम भाग-दौड़ करने लगे।
यह खुशी आन्तरिक है, यह समझ में आया उनकी चंचलता से ही।
फिर पुकार उठे, ''ओ सुशीला, कान बन्द कर रखे हैं क्या?'' तब तक सुशीला आकर खड़ी हो गयी।
यही है सुशीला!
हैरान होकर देखता रहा।
इन्हीं के लिए एक आदमी युगों से परिवार में अशान्ति झेल रहा है, समाज से बदनामी ले रहा है, अर्थ-सामर्थ्य जुटा रहा है। और अब जीवन के किनारे आकर भी सगे-सम्बन्धी, बच्चे, पड़ोसी सबके आगे सर झुका रहा है।
साँवली, पतली, लम्बी-सी एक बूढ़ी औरत, बाल छँटे हुए, सामने के दो दाँत गायब।
उसी पोपले चेहरे से हँसकर माँ से कहा उन्होंने, ''तू तो बेटे के पास विदेश में रहती है, नहीं? कब आयी? ओ मा! यही बेटा है क्या? बिलू या कुछ नाम था बचपन में?''
''बिलू नहीं, बोलू। अरे! इतना सब याद है तुम्हें, सुशीला दी?'' कह कर आराम से जिस पाप को झाड़ू मारकर विदा करने का दृढ़ संकल्प लेकर आ धमकी थी, उसी पाप के चरणों में माथा टेक दिया माँ ने।
''रहने दे, आ बैठ। रहेगी न थोड़े दिन?''
''नहीं, रहूँ तो कैसे?'' माँ ने अफसोस किया, ''बेटे की छुट्टियाँ तो गिनी-चुनी हैं।''
शायद और भी कुछ कहती मगर तब तक वीरू मामा ने हंगामा कर दिया, ''अच्छा, अच्छा, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले इनके हाथ-मुँह धोने का इन्तजाम कर दे। एक बार बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम नहीं।''
''जानती है बुलबुलि। तेरी यह सुशीलादी आज तुझे रात को सोने नहीं देगी। देखना, तुझे गाँव के इन तीस वर्षों की सारी बात बताकर छोड़ेगी। खबर भी तो रखती है सबकी।''
आतिथ्य-सत्कार के लिए तत्पर हो उठे वीरू मामा। किसी का कहना नहीं माने, चिलचिलाती धूप में खुद गये मिठाई खरीदने। कहीं किसी मछुआरिन को बोल आये, जैसे भी हो कुछ मछली का इन्तजाम करके लाये। और लोटते ही सुशीला के पीछे पड़ गये, ''तुझे हो क्या गया रे? दो आदमी का भोजन पकाने में बुड्ढी हो गयी तू?''
हम जितना भी परेशान होने को मना करते रहे, उतना ही परेशान होते गये वह।
यह घूस थी, या फिर अभिनय?
मगर माँ को क्या हो गया था? क्या वह भी अभिनय कर रही थीं?
मैं देख रहा था और हैरान हो रहा था।
मज़ेदार बात यह कि एक बार भी माँ मेरी तरफ़ नज़र नहीं कर रही थीं। सुनाई दे रहा था, चौके में जमकर बातें हो रही थीं, शायद उन्हीं तीस वर्षों का इतिहास वर्णित हो रहा था। कितने अनजाने नाम आकर कानों में गूँज रहे थे। सोच रहा था, कितने आश्चर्य की बात है। इतने लम्बे अरसे तक भारत के दूसरे छोर पर बिताकर भी माँ ने मन के भीतर बारूईपुर के प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षित रखा था।
इन तीस वर्षों में मैं न सही, माँ एक आध बार आ चुकी हैं। उसी का उल्लेख है माँ की बातों में, उस बार जब आई थी सुशीलादी, बाप रे! घर देखकर तो रोना ही आ गया था। आँगन में जंगल, दीवारें पलस्तर झरे हुए और चूहों के उपद्रव से घर-दालान सब तहस-नहस, चौके में दोनों चूल्हे जैसे मुँह के बल गिर पड़े हों, तुलसी मंच का पौधा सूखकर काठ, क्या भयंकर दृश्य था।
इस बार आकर दिल को चैन मिला। वही पुराना घर मगर इतना साफ कि सिन्दूर भी गिरे तो उठा लो। शुरू से ही से मेहनती हो तुम।
क्या सुशीलादी को कोई मन्त्र आता है? वशीकरण मन्त्र? क्या उसी मंत्र के सहारे ही वीरू मामा को...?
मगर वीरू मामा ने मंत्र के गुणों की बात नहीं की, बात की-हाथ के गुणों की।
मुझे साथ लेकर खाने बैठे, वही उनका मलाई से निकाला हुआ घी, घर की गाय के दूध की खीर, तालाब से पकड़ी मछली की तरकारी, बाग से तोड़कर लायी हुई सब्जियाँ, चटनी, सारे व्यंजनों के साथ। और मुझसे तीन गुना अधिक चट कर गये। फिर उँगली चाटते-चाटते प्रसन्नचित्त होकर अपनी छोटी बहन की ओर देखकर बोले, ''हाथ के जादू से, समझी बुलबुलि, सुशीला के हाथ के जादू से साग भी अमृत लगता है। जो कुछ पकाती, वही अमृत हो जाता है। उसके हाथ का पकाया भोजन खाने से बीमारी छूट जाती है, आयु बढ़ जाती है। मुझे ही देख ले, मैं अड़सठ वर्ष पार करने चला, देखकर लगता है क्या?''
माँ हँस पड़ी, ''सो तो नहीं लगता।''
वीरू मामा प्रोत्साहित होकर बोलने लगे, ''तभी तो घर-बार ठीक से बनवा लिया है मैंने। बिना परेशानी के और बीस साल जिन्दा रहूँगा मैं, देख लेना।''
वीरू मामा को जीने की इतनी चाहत क्यों है? लगता है, इसी चाहत के बल पर अभी काफ़ी दिन जिन्दा रहेंगे वह।
मगर किसी तरह भी यह आदमी पापी, शैतान, दुश्चरित्र या अपवित्र क्यों नहीं लग रहा है?
ऐसा सोचने को जी भी नहीं करता है।
क्या माँ की भी यही मन:स्थिति है?
तभी तो वीरू मामा की बात सुनकर हँसकर बोलीं, ''मुझे देखने को मत ही कहो वीरू भैया, देखना हो तो ऊपर से देख लूँगी।
''तुम औरतों का तो बस एक ही राग है। अब क्या जीना। जीकर क्या करना, क्यों भई? मगर बातों ही बातों में दिन ढलने चला। अच्छा सुशीला, तेरी अक्ल को क्या हो गया? तुझे तो सारे-सारे दिन भूख नहीं लगती है, ये शहरी लोग हैं, समय पर खाने की आदत है। लो, साथ में खुद भी थोड़ा-बहुत निगल जाओ, और देर करने की जरूरत नहीं है। चलो बोलू, हम लोग बैठक में जाकर बैठते है।''...दो कदम जाकर फिर ठिठककर रुक गये वीरू मामा। बोले, ''अपने लिए कुछ रखा है बचाकर या निरामिष भोजन भी सब हमें ही दे दिया तूने?''
जब से आया था, वीरू मामा की चीख-पुकार ही सुनी थी। सुशीलादी के साथ उन्हें बात करते पहली बार सुना। शान्त गम्भीर स्वर में सुशीलादी बोली, ''तुम जाते हो बैठक में?-''हाँ, हाँ, जाता ही हूँ।'' कहकर जल्दी से मुझे भगाकर ले आये वीरू मामा। लौटते समय ट्रेन में चढ़कर मैंने कहा, ''यह क्या हुआ माँ?'' मैके से निकलकर माँ का मन उदास था। उसी स्वर में बोलीं, ''हुआ ही क्या?''
''नीतू भैया को जाकर क्या कहोगी?
''कहूँगी क्या?'' अपनी आदत के अनुसार अचानक उत्तेजित होकर बोली, ''कहूँगी, क्यों वीरू भैया गाँव से हिलेंगे? इतना आदर, उनकी इतनी सेवा और कौन करेगा इस दुनिया में?
''माँ, कुछ अलग राग अलापने लगीं?''
माँ और भी उदास होकर बोलीं, ''तो क्या करूँ? हमेशा एक ही रागिनी बजती है क्या?''
''नीतू भैया कहेंगे तुमने घूस ली है।''
''ओह, कहैगा तो मैं डर से मर जाऊँगी। नीतू जज है क्या? और मैं चोर? मैं कहती हूँ, वह औरत जो अपार बुद्धि, शक्ति, और सेहत लेकर जीवन-भर यहाँ से वहाँ भटकती रही और दूसरों के घर में बेगारी करती रही, आज जीवन के अन्तिम काल में एक घर पाकर निहाल हो गयी है वह। बेचारी को उस आश्रय से उखाड़ कर फिर से निराश्रय कर दूँ? क्या सोचकर दया नहीं आती? किस तरह से इस घर को सजाया है, सँवारा है उसने। देखकर दिल भर जाता है। किस तरह मुँह पर कह दूँ, ''इस घर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम निकल जाओ।''
''मगर तुम्हारा समाज?''
''भाड़ में जाए समाज। आज समाज को मानता ही कौन है?''
-''और पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म?''
माँ ने एक लम्बी साँस छोड़कर कहा, ''देख बिलू गयी तो थी दौड़कर, मगर उन्हें देखकर लगा, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म का विचार करनेवाले हम कौन हैं? जो मालिक है, जो विचारकर्ता है, वही सत्य विचार करेंगे और तेरे वह बीरू मामा? उनका जो स्वभाव है, केवल सेवा-जतन के लिए ही नहीं, दिन-भर उनके फटकार सुनने के लिए भी किसी का होना जरूरी है। बेटों से होगा यह काम? बहुओं से? किसी से नहीं होगा। केवल वही कर पाएगा यह सब जिसने उसी पर अपनी जान न्योछावर की है।''
अपने आवेग को संयमित कर अचानक चुप हो गयीं माँ।
मैंने कहा, ''मगर मैंने तो कह दिया उनसे।''
''क्या कहा? किससे क्या कहा तूने?''
''वहाँ, तुम्हारे वीरू भैया को। मैंने कहा, इस तरह यहाँ अकेले रहने के कारण उनके बेटे बहुत दुःखी हैं। दस लोग उन्हीं की निन्दा करते हैं। कहते हैं बूढ़े बाप को छोड़ दिया...।''
''तो क्या? क्या जवाब दिया उन्होंने? लज्जित हुए या कि डाँटने लगे?''
''लज्जित नहीं हुए, डाँटा भी नहीं उन्होंने।'' ठण्डी आवाज़ में बोले, ''ये मैं नहीं समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है बेटा। मगर सोचकर देखो, मैं यहाँ रहता हूँ तभी तो सुशीला को दो वक्त का खाना मिल रहा है। मेरे बेटे उसे माहवार खर्चा देंगे क्या? मेरी नौकरी नहीं रही, नकद रुपये देने की क्षमता नहीं, इसीलिए यह चक्कर चला कर बैठा हूँ। जीवन-भर जो मेरे आसरे पर ही जीती रही, उसे अब 'मेरे पास रुपये नहीं' कहकर भगा दूँ? और उसे भी 'जीवन-भर अपना एक घर नहीं बना' यही आक्षेप रह गया। तभी कहता हूँ, कुछ भी तो नहीं मिला उसे। कम-से-कम मरने से पहले कड़ाही-करछी हिलाकर अगर जीवन सार्थक लगे, दिल को चैन मिले तो वही सही। बेटों से तो कह दिया मैंने, तुम लोग जी खोलकर मेरी निन्दा कर लो। कहना बाबूजी बदमिज़ाजी हैं, सनकी हैं, बाबूजी जिद्दी हैं, चिड़चिड़े हैं, किसी के साथ मिल-जुलकर नहीं रह पाते हैं। नहीं तो और भी जो जी चाहे कह देना लोगों से, मुझे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा।''
क्या माँ को ठीक से सब सुनाई पड़ा? देख रहा हूँ खिड़की से बाहर की ओर मुँह करके बैठी हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i