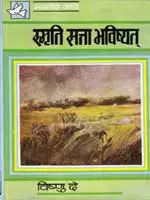|
कविता संग्रह >> स्मृति सत्ता भविष्यत् स्मृति सत्ता भविष्यत्विष्णु दे
|
355 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत हैं कविताएँ...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
विष्णु दे का रचना-वितानः प्रस्तुति एवं प्रस्थान
डॉ. रणजीत साहा
विष्णु दे (1909-1984 ई.) के काव्य जीवन की शुरूआत निजी पीड़ा और एकान्त
के दंश से शुरू हुई। उनका यह निजत्व निसंग, जो अपने एकाकी स्वभाव से जुड़ा
था, धीरे-धीरे निसर्ग में विसर्जन हो गया। अपने आरंभिक लेखन के दौर में
स्वयं को प्रकाशित करने की भावना का जहाँ अभाव था- वहाँ उस गोपन में
भी-अस्तित्व को जुगाये रखने का संकट आड़े आ गया। आत्म सचेतन होने की
प्रक्रिया में। जहाँ वह टी. एस. एलियट से जुड़ें वही प्रमथ चौधुरी
(1868-1946) की रचनाओं ने भी उन पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन आत्म सजगता और
वृहत्तर ऐतिह्य--बोध उन्हें किसी भी सीमा रेखा में या प्रभाव वृत्त में
बाँध या समेट न पाया। उन्हें ऐसा जरूर लगने लगा था कि ‘मनुष्यों
के
जंगल में एक परदेशी सैलानी की तरह वह अपने आत्म-प्रत्यय के लिए भटक रहे
हैं।
यही भटकाव और तलाश उन्हें मार्क्सवाद के निकट ले आयी और तब उन्हें प्रतीत होने लगा कि उनके कवि व्यक्तित्व को आंशिक आश्वस्ति मिली है। वह दौर था जब ‘उर्वशी और आर्टेमिस’ (1933) तथा ‘चोरा बालि’ (1947) की कविताएं लिखी जाने को थीं। स्वाध्याय के प्रति गहरी रूझान और सामाजिक दायित्व बोध के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा ने उनके आत्म संसार को और आदिगंत व्याप्त चेतना से जुड़े विचारों ने स्वभावतः और अनिवार्यतः उन पर प्रभाव डाला, और यह विचार धारा उनकी काव्य-मनीषा की अपरिहार्य अंग बन गयी। इस विचार सरणी में उनके साथ और भी कई कवि सम्मलित थे, जिनमें अरुण मिश्र (जन्म 1909) और सुभाष मुखोपाध्याय (जन्म 1919) प्रतिनिधि नाम हैं, और जिनकी लेखनी आज भी सक्रिय है।
तत्कालीन साहित्यकार मंच पर अपने लेखक मित्रों और समकालीन कवियों के साथ दीखते हुए भी विष्णु दे सबसे अलग रहे। अपनी आरंभिक रचना, जो कि एक कहानी थी ‘पुराणेर पुनर्जन्म या लक्षण’ शीर्षक से (ढाका से प्रकाशित होनेवाली प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका ‘प्रगति’ में) 1928 में छपी थी। इसके बाद 1931 में ‘परिचय’ प्रथम अंक में ही उनकी दो कविताएँ छपी थीं। इसी अंक में मार्सल प्रूस्त की एक कविता का अनुवाद भी छपा था। ‘उर्वशी और आर्टेमिस’ इस काव्य-रूपक से ही स्पष्ट है कि काव्य चेतना के स्तर पर वे नवीन प्रयोगों के पक्षधर थे। उर्वशी इन्द्रलोक की प्रसिद्ध अप्सरा थी जो शापवश भूलोक में पुरूरवा की प्रेयसी और पत्नी बनकर रही और केन्द्रीय पात्रा के रूप में इस पर कई कृतियां लिखी गयीं। ‘आर्टेमस ग्रीक गाथा की एक प्रसिद्ध पात्रा थी, जो अपने भाई अपोलो के साथ ओलिम्पस के प्रमुख बारह देव-देवी मंडल में प्रतिष्ठित थी और जिसने अक्षत कुमारी बने रहने का वरदान पाया था। वह आखेट की देवी के रूप में भी मान्य है। इस अपूर्व सुन्दरी को झील में विवस्त्र देख पाने का सौभाग्य ऐक्टेयॉन को मिला था लेकिन वह आर्टेमिस के शाप से हिरण में परिणित हो गया। उस पर शिकारी कुत्तों ने धावा बोल दिया और उसे चीर-फाड़ कर खा गये। इस विवरण से स्पष्ट है कि सामान्तर मिथकों के विनियोग द्वारा विष्णु दे अपनी काव्य चेतना को सार्वजनिक विस्तार देना चाहते थे और अपने समकालीनों से विशिष्ट होने की तैयारी में उनके अपने स्वभाव और स्वाध्याय ने भी बहुत योगदान किया और इससे उनकी आत्मोन्मुखी वृत्तियों को समुचित विस्तार भी मिला।
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (1861-1941) और काजी नजरूल इस्लाम (1899-1976) जो क्रमशः भारतीय मनीषा के संस्कृति पुरुष तथा सामाजिक चेतना के प्रतीक और ‘अग्निवीणा’ वादक थे, ने विष्णु दे को प्रभावित अवश्य किया था लेकिन यह प्रभाव आंशिक ही था। इस बात पर उनके आलोचकों में बहस की जाती रही है कि स्वयं रवीन्द्रनाथ को विष्णु दे ने कहाँ तक और कितनी दूर तक सराहा था। विष्णु दे ने अपने यौवन में ही इस बात को लक्ष्य किया था कि ‘कल्लोल गोष्ठी’ के कवि-आलोचकों और समर्थकों द्वारा रवीन्द्रनाथ के मूर्तिभंजन का प्रयास किस तरह एक षड्यन्त्र में बदल चुका है और रवीन्द्र नाथ इससे बुरी तरह आहात भी थे। लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप अस्तित्ववादी दर्शन से जुड़े रहने और इसके प्रवक्ता होने के कारण और अन्यान्य दर्शनों या मतवादों (यथा अद्वैत और विश्व-मानवतावाद) के पुरोधा एवं प्रशंसक होने के नाते रवीन्द्रनाथ विष्णु दे के लिए सदैव आदरणीय बने रहे। अपने युगोचित उत्साह में अन्य कवियों की तरह उन्होंने रवीन्द्रनाथ की सार्वभौमिक और सार्वकालिक उपस्थिति की संवर्धना की। बाद में अपने एक काव्य संकलन ‘तुमि शुधु पंचिसे बैसाख’ (1958; ‘क्या तुम केवल वैशाख माह की पचीसवीं तिथि हो’-रवीन्द्रनाथ का जन्म दिन) में उन्होंने लोगों की उस मानसिकता का विरोध किया था जो कवियों का जन्मदिन मनाकर ही अपने कर्तव्य और दायित्व की इतिश्री मान लेते हैं।
दरअसल अपने पूर्ववर्ती और समकालीन कवियों के प्रशंसक होने और उनका नैकट्य पाने के बावजूद विष्णु दे ने अपनी शर्तों पर एक कवि और समग्र कविशिल्पी का जीवन जिया। बाद में, पॉल एलुयार, लुई आँराग और पाब्लो नेरुदा की मानवता संघर्षशील चेतना ने विष्णु दे के काव्य-क्षितिज को और भी विस्तार दिया। लेकिन अपनी भारतीय पृष्ठभूमि-आधारभूत ग्रथों (जिसमें शास्त्र-पुराण, गाथाएँ सभी सम्मिलित हैं।) का चिंतन-मनन, उन्हें उन पौराणिक एवं मिथकीय संदर्भों को और भी परिचित कराने में सहायक हो सका जो साहित्य में प्रतीक और अभिप्राय के बतौर बार-बार प्रयुक्त होते रहे थे। भारतीय मिथकों के समानान्तर विश्व की विभिन्न सांस्कृतियों में प्राप्त गाथाओं और समानधर्मी दृष्टान्तों की पड़ताल से उनका काव्य जगत् नयी उद्भावनाओं से व्यंजित हो सका।
लेकिन समसामायिक राजनैतिक परिवर्तनों और संदर्भों से भी उनके परिचय का दायरा निरंतर बढ़ता गया। काव्य-प्रणयन के आरंभिक चरण में इन हवालों से बोझिल उनकी पंक्तियाँ अपने जटिल और संदर्भ-गझिन विधान से अपने पाठकों को अवश्य ही चमत्कृत करती थीं। कहना चाहिए, आंतकित भी करती थीं लेकिन 1950 में प्रकाशित ‘अन्विष्ट’ काव्य-संकलन की कविताएँ इन आयोजनों और उपक्रमों के जटाजाल से मुक्त जान पड़ती हैं। अपनी परवर्ती रचनाओं ‘नाम रेखेछि कोमल गान्धार’ (1953), ‘आलेख्य’ (1958) ‘स्मृति सत्ता भविष्यत्’ (1963), ‘एकूश-बाइस’ (1953), ‘सेई अंधकार चाइ’ (1966), ‘रवि करोज्जल निजदेश’ (1973), ‘ईशावास्य दिवानिशा’ (1974), ‘चित्ररूपमत्त पृथिवीर’ (1976), ‘उत्तरे थाको मौन’ (1977) में उनका स्वर क्रमशः संयत, पारदर्शी और अनाडम्बरपूर्ण होता चला गया। इन संकलनों में उनका द्रष्टारूप अधिक मुखर है जबकि कविरूप अधिक मौन और गम्भीर होता चला गया है।
अपने सरोकारों के प्रति चौकस लेकिन अपने ईर्द-गिर्द चलनेवाले छोटे-बड़े साहित्यक आन्दोलनों एवं राजनैतिक धड़ों से अगल विष्णु दे की काव्य-चेतना भूमि और भूमा को समर्पित रही। सामाजिक शोषण, अन्याय, श्रेणी विभाजन, वैषम्य आदि पर जहाँ वह करारा प्रहर करते हैं वहाँ काव्य की मर्यादाओं का भी बराबर रखते हैं। उसे वे नारेबाजी और पार्टी का हलफनामा नहीं बनाते। साथ ही, उन पर आरोप भी नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने सर्वहारा या आम जनता के हक की अनदेखी की-इस दृष्टि से उनकी सारी रचनाएँ शोषण, गरीबी, हताशा और वर्ग भेद के विरुद्ध आम आदमी के एकजुट होने का आह्वान करती है। इस अभियान-क्रम के दौर में ही कवि ने ‘लाल तारा’ जैसी कविता लिखी थी, जो उनके प्रसिद्ध काव्य-संकलन ‘सन्द्वीपेर चर’ में संकलित है। इसमें उच्चैः श्रवा की ह्रेषाध्वनि और पक्षीराज की उड़ान को प्रतीक रूप में ग्रहण किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि इस कविता को साम्यावादी विचार-धारा की सशक्त एवं प्रतिनिधि रचना के रूप रखा जाता रहा है लेकिन अपनी परम्परागत विजय यात्रा और देश के लोगों के जयगान को ही कवि ने सर्वाधिक महत्त्व दिया है-
यही भटकाव और तलाश उन्हें मार्क्सवाद के निकट ले आयी और तब उन्हें प्रतीत होने लगा कि उनके कवि व्यक्तित्व को आंशिक आश्वस्ति मिली है। वह दौर था जब ‘उर्वशी और आर्टेमिस’ (1933) तथा ‘चोरा बालि’ (1947) की कविताएं लिखी जाने को थीं। स्वाध्याय के प्रति गहरी रूझान और सामाजिक दायित्व बोध के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा ने उनके आत्म संसार को और आदिगंत व्याप्त चेतना से जुड़े विचारों ने स्वभावतः और अनिवार्यतः उन पर प्रभाव डाला, और यह विचार धारा उनकी काव्य-मनीषा की अपरिहार्य अंग बन गयी। इस विचार सरणी में उनके साथ और भी कई कवि सम्मलित थे, जिनमें अरुण मिश्र (जन्म 1909) और सुभाष मुखोपाध्याय (जन्म 1919) प्रतिनिधि नाम हैं, और जिनकी लेखनी आज भी सक्रिय है।
तत्कालीन साहित्यकार मंच पर अपने लेखक मित्रों और समकालीन कवियों के साथ दीखते हुए भी विष्णु दे सबसे अलग रहे। अपनी आरंभिक रचना, जो कि एक कहानी थी ‘पुराणेर पुनर्जन्म या लक्षण’ शीर्षक से (ढाका से प्रकाशित होनेवाली प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका ‘प्रगति’ में) 1928 में छपी थी। इसके बाद 1931 में ‘परिचय’ प्रथम अंक में ही उनकी दो कविताएँ छपी थीं। इसी अंक में मार्सल प्रूस्त की एक कविता का अनुवाद भी छपा था। ‘उर्वशी और आर्टेमिस’ इस काव्य-रूपक से ही स्पष्ट है कि काव्य चेतना के स्तर पर वे नवीन प्रयोगों के पक्षधर थे। उर्वशी इन्द्रलोक की प्रसिद्ध अप्सरा थी जो शापवश भूलोक में पुरूरवा की प्रेयसी और पत्नी बनकर रही और केन्द्रीय पात्रा के रूप में इस पर कई कृतियां लिखी गयीं। ‘आर्टेमस ग्रीक गाथा की एक प्रसिद्ध पात्रा थी, जो अपने भाई अपोलो के साथ ओलिम्पस के प्रमुख बारह देव-देवी मंडल में प्रतिष्ठित थी और जिसने अक्षत कुमारी बने रहने का वरदान पाया था। वह आखेट की देवी के रूप में भी मान्य है। इस अपूर्व सुन्दरी को झील में विवस्त्र देख पाने का सौभाग्य ऐक्टेयॉन को मिला था लेकिन वह आर्टेमिस के शाप से हिरण में परिणित हो गया। उस पर शिकारी कुत्तों ने धावा बोल दिया और उसे चीर-फाड़ कर खा गये। इस विवरण से स्पष्ट है कि सामान्तर मिथकों के विनियोग द्वारा विष्णु दे अपनी काव्य चेतना को सार्वजनिक विस्तार देना चाहते थे और अपने समकालीनों से विशिष्ट होने की तैयारी में उनके अपने स्वभाव और स्वाध्याय ने भी बहुत योगदान किया और इससे उनकी आत्मोन्मुखी वृत्तियों को समुचित विस्तार भी मिला।
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (1861-1941) और काजी नजरूल इस्लाम (1899-1976) जो क्रमशः भारतीय मनीषा के संस्कृति पुरुष तथा सामाजिक चेतना के प्रतीक और ‘अग्निवीणा’ वादक थे, ने विष्णु दे को प्रभावित अवश्य किया था लेकिन यह प्रभाव आंशिक ही था। इस बात पर उनके आलोचकों में बहस की जाती रही है कि स्वयं रवीन्द्रनाथ को विष्णु दे ने कहाँ तक और कितनी दूर तक सराहा था। विष्णु दे ने अपने यौवन में ही इस बात को लक्ष्य किया था कि ‘कल्लोल गोष्ठी’ के कवि-आलोचकों और समर्थकों द्वारा रवीन्द्रनाथ के मूर्तिभंजन का प्रयास किस तरह एक षड्यन्त्र में बदल चुका है और रवीन्द्र नाथ इससे बुरी तरह आहात भी थे। लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप अस्तित्ववादी दर्शन से जुड़े रहने और इसके प्रवक्ता होने के कारण और अन्यान्य दर्शनों या मतवादों (यथा अद्वैत और विश्व-मानवतावाद) के पुरोधा एवं प्रशंसक होने के नाते रवीन्द्रनाथ विष्णु दे के लिए सदैव आदरणीय बने रहे। अपने युगोचित उत्साह में अन्य कवियों की तरह उन्होंने रवीन्द्रनाथ की सार्वभौमिक और सार्वकालिक उपस्थिति की संवर्धना की। बाद में अपने एक काव्य संकलन ‘तुमि शुधु पंचिसे बैसाख’ (1958; ‘क्या तुम केवल वैशाख माह की पचीसवीं तिथि हो’-रवीन्द्रनाथ का जन्म दिन) में उन्होंने लोगों की उस मानसिकता का विरोध किया था जो कवियों का जन्मदिन मनाकर ही अपने कर्तव्य और दायित्व की इतिश्री मान लेते हैं।
दरअसल अपने पूर्ववर्ती और समकालीन कवियों के प्रशंसक होने और उनका नैकट्य पाने के बावजूद विष्णु दे ने अपनी शर्तों पर एक कवि और समग्र कविशिल्पी का जीवन जिया। बाद में, पॉल एलुयार, लुई आँराग और पाब्लो नेरुदा की मानवता संघर्षशील चेतना ने विष्णु दे के काव्य-क्षितिज को और भी विस्तार दिया। लेकिन अपनी भारतीय पृष्ठभूमि-आधारभूत ग्रथों (जिसमें शास्त्र-पुराण, गाथाएँ सभी सम्मिलित हैं।) का चिंतन-मनन, उन्हें उन पौराणिक एवं मिथकीय संदर्भों को और भी परिचित कराने में सहायक हो सका जो साहित्य में प्रतीक और अभिप्राय के बतौर बार-बार प्रयुक्त होते रहे थे। भारतीय मिथकों के समानान्तर विश्व की विभिन्न सांस्कृतियों में प्राप्त गाथाओं और समानधर्मी दृष्टान्तों की पड़ताल से उनका काव्य जगत् नयी उद्भावनाओं से व्यंजित हो सका।
लेकिन समसामायिक राजनैतिक परिवर्तनों और संदर्भों से भी उनके परिचय का दायरा निरंतर बढ़ता गया। काव्य-प्रणयन के आरंभिक चरण में इन हवालों से बोझिल उनकी पंक्तियाँ अपने जटिल और संदर्भ-गझिन विधान से अपने पाठकों को अवश्य ही चमत्कृत करती थीं। कहना चाहिए, आंतकित भी करती थीं लेकिन 1950 में प्रकाशित ‘अन्विष्ट’ काव्य-संकलन की कविताएँ इन आयोजनों और उपक्रमों के जटाजाल से मुक्त जान पड़ती हैं। अपनी परवर्ती रचनाओं ‘नाम रेखेछि कोमल गान्धार’ (1953), ‘आलेख्य’ (1958) ‘स्मृति सत्ता भविष्यत्’ (1963), ‘एकूश-बाइस’ (1953), ‘सेई अंधकार चाइ’ (1966), ‘रवि करोज्जल निजदेश’ (1973), ‘ईशावास्य दिवानिशा’ (1974), ‘चित्ररूपमत्त पृथिवीर’ (1976), ‘उत्तरे थाको मौन’ (1977) में उनका स्वर क्रमशः संयत, पारदर्शी और अनाडम्बरपूर्ण होता चला गया। इन संकलनों में उनका द्रष्टारूप अधिक मुखर है जबकि कविरूप अधिक मौन और गम्भीर होता चला गया है।
अपने सरोकारों के प्रति चौकस लेकिन अपने ईर्द-गिर्द चलनेवाले छोटे-बड़े साहित्यक आन्दोलनों एवं राजनैतिक धड़ों से अगल विष्णु दे की काव्य-चेतना भूमि और भूमा को समर्पित रही। सामाजिक शोषण, अन्याय, श्रेणी विभाजन, वैषम्य आदि पर जहाँ वह करारा प्रहर करते हैं वहाँ काव्य की मर्यादाओं का भी बराबर रखते हैं। उसे वे नारेबाजी और पार्टी का हलफनामा नहीं बनाते। साथ ही, उन पर आरोप भी नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने सर्वहारा या आम जनता के हक की अनदेखी की-इस दृष्टि से उनकी सारी रचनाएँ शोषण, गरीबी, हताशा और वर्ग भेद के विरुद्ध आम आदमी के एकजुट होने का आह्वान करती है। इस अभियान-क्रम के दौर में ही कवि ने ‘लाल तारा’ जैसी कविता लिखी थी, जो उनके प्रसिद्ध काव्य-संकलन ‘सन्द्वीपेर चर’ में संकलित है। इसमें उच्चैः श्रवा की ह्रेषाध्वनि और पक्षीराज की उड़ान को प्रतीक रूप में ग्रहण किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि इस कविता को साम्यावादी विचार-धारा की सशक्त एवं प्रतिनिधि रचना के रूप रखा जाता रहा है लेकिन अपनी परम्परागत विजय यात्रा और देश के लोगों के जयगान को ही कवि ने सर्वाधिक महत्त्व दिया है-
‘‘गिरी नहीं गिरेगी भी नहीं, तुम्हारे घोड़े की नाल
प्राणों के इस्पात से सुदृढ़ तुम्हारा अभियान—
भीरु बन्धुओं के देश में तभी तो
तुम्हारी उन दुर्जन भुजाओं ने गुंजाया जयगान।’’
प्राणों के इस्पात से सुदृढ़ तुम्हारा अभियान—
भीरु बन्धुओं के देश में तभी तो
तुम्हारी उन दुर्जन भुजाओं ने गुंजाया जयगान।’’
(लाल तारा/ सन्द्वीपेर चर)
ऐसी पंक्तियों की संख्या न तो कम है और न उसमें दोहराव ही आया है। उनकी
कविताओं में जो वैविध्य है और जितने आयाम हैं वे पाठकों और समीक्षकों को
सचमुच हैरानी में डालनेवाले हैं। यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ युग की ठीक
बाद वाली पीढ़ी में वे शीर्षस्थानीय कवि-चिंतक के रूप में समादृत हो सके।
जब उनके समकालीन कुछ अन्य कवि इस जघन्य धरती पर व्याप्त निराशा, हताशा,
स्वच्छन्दता के नाम पर आत्म-पलायन, मुक्ति के नाम पर विकृत यौनाचारों को
प्रश्रय दे रहे थे और सारे मूल्यों की अवमानना का काव्योत्सव मना रहे थे
उस समय विष्णु दे और उन सरीखें समाजचेता कवियों ने व्यक्ति और समाज की
पीड़ा, आशा और आकांक्षा, ताप और अनुताप, दाह और दंश को वाणी दी तथा
सामाजिक न्याय के साथ व्यक्ति को उसके स्वत्रतंत्र आत्म-निर्णय
के
अधिकार से जोड़ा।
लेकिन समान उद्देश्यों और साधनों के बावजूद ऐसे भी बहुत-से कवि थे जो अपनी-अपनी प्रतिज्ञा और प्रतिबद्धता के बावजूद अन्यत्र और अन्यथा व्यस्त होते चले गये। उदाहरण के लिए, सुधीन्द्रनाथ दत्त (1901-1960) जन-जन के आक्रोश से बचने की ख़ातिर नेतिवाद के आश्रय में चले गये। बुद्धदेव बसु (1903-1976) कलावाद के अनन्य प्रवक्ता बन गये और कवि जीवन के अभ्युदय काल में उन्होंने जिन काव्य धारणाओं का सक्रिय विरोध किया था। क्रमशः वे उन्हीं प्रस्थानों या अभिगमों की ओर लौट गये। अमिय चक्रवर्ती (1901-1986) ने काल के अखंड चेतना को निश्चित संदर्भों में एक सीमा तक पकड़ा था लेकिन बाद में विज्ञानवादी अवधारणाओं के साथ अतीन्द्रियता के तालमेल बिठाने के क्रम में उनके काव्य की दिशा खो गयी; कहना चाहिए, दृष्टि खो गयी।
सर्वश्री अचिन्त्य कुमार सेनगुप्त, बुद्धदेव बसु मोहितलाल मजूमदार, काजी नजरुल इस्लाम के साथ युवा कवियों और लेखकों का मण्डल ‘कल्लोल गोष्ठी’ से सम्बद्ध हुआ लेकिन बाद में सबकी दिशाएँ अलग-अलग हो गयीं। इनमें से हर एक ने साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया। सेनगुप्त, बोस और मजुमदार की यह ‘त्रयी’ बहुत चर्चित भी हुई लेकिन बाद में ‘कल्लोल गोष्ठी’ के दूसरे सदस्यों और नये प्रगतिशील वर्ग के निन्दकों द्वारा ही इसे बदनाम किया जाने लगा।
प्रेमेन्द्र मित्र (1904-1988) जो कल्लोल युग के विशिष्ट कवि थे। ह्विटमैन आदि के प्रभाव में मानव के गौरवपूर्ण वर्तमान और मानवीय अभीप्सा को स्वर दे रहे थे और इस दृष्टि से लम्बे समय तक प्रासंगिक बने रहे। उनका पहला काव्य-संकलन ‘पाओंदल’ (1925) लाखों-करोंड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करनेवाली एक विशिष्ट कृति थी और परवर्ती कृतियों में भी उनका लोक-संकल्प अधिकाधिक मुखर होता चला गया।
अपनी आरंभिक रचनाओं से चर्चित हो जाने वाले विष्णु दे की ‘अन्विष्ट’ और ‘आलेख्य’ काव्य-कृतियों ने उन्हें ने उन्हें बाङ्ला काव्य-सागर में पूरी तरह प्रतिष्ठित कर दिया। उनकी परवर्ती रचनाओं में उनकी सर्वश्रेष्ठ लंबी कविता ‘स्मृति सत्ता भविष्य’ वर्ण 1971 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित किया गया। इस सम्मान के पूर्व ‘स्मृति सत्ता भविष्यत्’ काव्य-संकलन को वर्ष 1963 की सर्वश्रेष्ठ बाङ्ला कृति होने के नाते केन्द्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। इस संकलन में कवि-मनीषी विष्णु दे की 1955 से 1961 तक की कविताएँ संकलित हैं। अकादमी पुरस्कार की प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख किया गया कि ‘स्मृति सत्ता भविष्यत्’ कविता कवि के सर्जक व्यक्तित्व का अगला सोपान है, जिसमें उसके निजी एकान्त के साथ उसके परिवेश का गहरा तादात्म्य पूरी अंतरंगता से अंकित है। इस सम्मान में उन्हें सर्वभारतीय स्वपूप प्रदान किया जो इसी नाम के संकलन (1963) में संकलित थी। 234 पंक्तियों में संयोजित भाव-विचार-बिम्बों से समृद्ध लम्बी कविता हमारी खोयी हुई पहचान का मुखर दास्तावेज़ है। इस कविता में आत्म परिचय के लिए संधान में निकले कवि ने हमारी विडम्बनाओं और सामाजिक विवृत्तियों के ढेर सारे परस्पर विरोधी चित्र उकेरे हैं।
कहना चाहिए कि इस कौशल से जुटाये हैं उनके सारे आशय और अभिप्राय अपने कथन के साथ एक नयी गूँज पैदा करते हैं। यह लम्बी कविता हमारी कुठा, कुत्सा, विकृत और विद्रूप मानसिकता से ग्रस्त उस समाज को प्रस्तुत करती है यहाँ व्यक्ति और संस्था दोनों ही अपनी-अपनी पहचान खोकर इसे फिर से पाने की तैयारियों में लगे हैं। जहाँ न तो साधन की पवित्रता है और न कोई सकारात्मक संकल्प और ना ही कोई दिशा। अपने ऐतिह्य और संस्कृति बोध के कट जाने की पीड़ा और सामूहिक चेतना से विच्छिन्न और विभक्त व्यक्तिवाद और निरंकुश आचरण ने कवि के चित्त में एक खिन्नता भरा तिक्त अवसाद पैदा कर दिया है।
वह अपने सामने खड़ी उस नवीन या वर्तमान पीढ़ी से कई सवाल पूछता है जो दिशाहीन है। देश के धुँधले दर्पण में प्रस्तुत पीढ़ी और बीस-बाइस वर्ष के युवाओं की आँखों में यह देश एक-दूसरे के लिए पूरी तरह अपरिचित हैं। ये युवा अपने को प्रवासी समझते हैं और स्वदेश की स्मृति उसके लिए विलास है। उनके लिए सोलह और अठारह मंजली इमारतों का वैभव ही सब कुछ है। लेकिन महानगर (कलकत्ता) के माथे पर कलंक के रूप में उगने वाले इन बेढंगे, बदसूरत और बेतरतीब कंक्रीट के जंगल के साथ-साथ यहाँ की कच्ची सड़कें, गंदी बस्तियाँ, तंग फुटपाथ, बदहाली भाषावाद, डरावने सपने, महामारी, अभाव रूदन, भूख, हड़ताल, बेकारी और निराशा का ही बोलबाला है। इस विषण्ण, अवसाद से भरे और चरम निराशा के माहौल को कवि ने इन पंक्तियों में रखा है।
लेकिन समान उद्देश्यों और साधनों के बावजूद ऐसे भी बहुत-से कवि थे जो अपनी-अपनी प्रतिज्ञा और प्रतिबद्धता के बावजूद अन्यत्र और अन्यथा व्यस्त होते चले गये। उदाहरण के लिए, सुधीन्द्रनाथ दत्त (1901-1960) जन-जन के आक्रोश से बचने की ख़ातिर नेतिवाद के आश्रय में चले गये। बुद्धदेव बसु (1903-1976) कलावाद के अनन्य प्रवक्ता बन गये और कवि जीवन के अभ्युदय काल में उन्होंने जिन काव्य धारणाओं का सक्रिय विरोध किया था। क्रमशः वे उन्हीं प्रस्थानों या अभिगमों की ओर लौट गये। अमिय चक्रवर्ती (1901-1986) ने काल के अखंड चेतना को निश्चित संदर्भों में एक सीमा तक पकड़ा था लेकिन बाद में विज्ञानवादी अवधारणाओं के साथ अतीन्द्रियता के तालमेल बिठाने के क्रम में उनके काव्य की दिशा खो गयी; कहना चाहिए, दृष्टि खो गयी।
सर्वश्री अचिन्त्य कुमार सेनगुप्त, बुद्धदेव बसु मोहितलाल मजूमदार, काजी नजरुल इस्लाम के साथ युवा कवियों और लेखकों का मण्डल ‘कल्लोल गोष्ठी’ से सम्बद्ध हुआ लेकिन बाद में सबकी दिशाएँ अलग-अलग हो गयीं। इनमें से हर एक ने साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया। सेनगुप्त, बोस और मजुमदार की यह ‘त्रयी’ बहुत चर्चित भी हुई लेकिन बाद में ‘कल्लोल गोष्ठी’ के दूसरे सदस्यों और नये प्रगतिशील वर्ग के निन्दकों द्वारा ही इसे बदनाम किया जाने लगा।
प्रेमेन्द्र मित्र (1904-1988) जो कल्लोल युग के विशिष्ट कवि थे। ह्विटमैन आदि के प्रभाव में मानव के गौरवपूर्ण वर्तमान और मानवीय अभीप्सा को स्वर दे रहे थे और इस दृष्टि से लम्बे समय तक प्रासंगिक बने रहे। उनका पहला काव्य-संकलन ‘पाओंदल’ (1925) लाखों-करोंड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करनेवाली एक विशिष्ट कृति थी और परवर्ती कृतियों में भी उनका लोक-संकल्प अधिकाधिक मुखर होता चला गया।
अपनी आरंभिक रचनाओं से चर्चित हो जाने वाले विष्णु दे की ‘अन्विष्ट’ और ‘आलेख्य’ काव्य-कृतियों ने उन्हें ने उन्हें बाङ्ला काव्य-सागर में पूरी तरह प्रतिष्ठित कर दिया। उनकी परवर्ती रचनाओं में उनकी सर्वश्रेष्ठ लंबी कविता ‘स्मृति सत्ता भविष्य’ वर्ण 1971 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित किया गया। इस सम्मान के पूर्व ‘स्मृति सत्ता भविष्यत्’ काव्य-संकलन को वर्ष 1963 की सर्वश्रेष्ठ बाङ्ला कृति होने के नाते केन्द्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। इस संकलन में कवि-मनीषी विष्णु दे की 1955 से 1961 तक की कविताएँ संकलित हैं। अकादमी पुरस्कार की प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख किया गया कि ‘स्मृति सत्ता भविष्यत्’ कविता कवि के सर्जक व्यक्तित्व का अगला सोपान है, जिसमें उसके निजी एकान्त के साथ उसके परिवेश का गहरा तादात्म्य पूरी अंतरंगता से अंकित है। इस सम्मान में उन्हें सर्वभारतीय स्वपूप प्रदान किया जो इसी नाम के संकलन (1963) में संकलित थी। 234 पंक्तियों में संयोजित भाव-विचार-बिम्बों से समृद्ध लम्बी कविता हमारी खोयी हुई पहचान का मुखर दास्तावेज़ है। इस कविता में आत्म परिचय के लिए संधान में निकले कवि ने हमारी विडम्बनाओं और सामाजिक विवृत्तियों के ढेर सारे परस्पर विरोधी चित्र उकेरे हैं।
कहना चाहिए कि इस कौशल से जुटाये हैं उनके सारे आशय और अभिप्राय अपने कथन के साथ एक नयी गूँज पैदा करते हैं। यह लम्बी कविता हमारी कुठा, कुत्सा, विकृत और विद्रूप मानसिकता से ग्रस्त उस समाज को प्रस्तुत करती है यहाँ व्यक्ति और संस्था दोनों ही अपनी-अपनी पहचान खोकर इसे फिर से पाने की तैयारियों में लगे हैं। जहाँ न तो साधन की पवित्रता है और न कोई सकारात्मक संकल्प और ना ही कोई दिशा। अपने ऐतिह्य और संस्कृति बोध के कट जाने की पीड़ा और सामूहिक चेतना से विच्छिन्न और विभक्त व्यक्तिवाद और निरंकुश आचरण ने कवि के चित्त में एक खिन्नता भरा तिक्त अवसाद पैदा कर दिया है।
वह अपने सामने खड़ी उस नवीन या वर्तमान पीढ़ी से कई सवाल पूछता है जो दिशाहीन है। देश के धुँधले दर्पण में प्रस्तुत पीढ़ी और बीस-बाइस वर्ष के युवाओं की आँखों में यह देश एक-दूसरे के लिए पूरी तरह अपरिचित हैं। ये युवा अपने को प्रवासी समझते हैं और स्वदेश की स्मृति उसके लिए विलास है। उनके लिए सोलह और अठारह मंजली इमारतों का वैभव ही सब कुछ है। लेकिन महानगर (कलकत्ता) के माथे पर कलंक के रूप में उगने वाले इन बेढंगे, बदसूरत और बेतरतीब कंक्रीट के जंगल के साथ-साथ यहाँ की कच्ची सड़कें, गंदी बस्तियाँ, तंग फुटपाथ, बदहाली भाषावाद, डरावने सपने, महामारी, अभाव रूदन, भूख, हड़ताल, बेकारी और निराशा का ही बोलबाला है। इस विषण्ण, अवसाद से भरे और चरम निराशा के माहौल को कवि ने इन पंक्तियों में रखा है।
‘‘बाँचबार आशा नेई, बाँचाबार भाषा नेई
से खाने मड़क अवरित
सेखाने कान्नार सुर एक घेये निर्जला अकाले
कारण कारोई कोनो आशा नेई
अथवा ता एत कम, जे कोनो निराशा नेई।’’.....
से खाने मड़क अवरित
सेखाने कान्नार सुर एक घेये निर्जला अकाले
कारण कारोई कोनो आशा नेई
अथवा ता एत कम, जे कोनो निराशा नेई।’’.....
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i