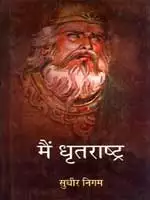|
पौराणिक >> मैं धृतराष्ट्र मैं धृतराष्ट्रसुधीर निगम
|
322 पाठक हैं |
|||||||
कई वर्षों के शोध-अनुसंधान पर आधारित श्री सुधीर निगम की एक अभिनव कृति...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘महाभारत’ के आदि पर्व में कहा गया है कि
‘‘धृतराष्ट्र ही मूल महाभारत की कथा के टूटे हुए तार
को पुनः
वीरकाव्योचित और गौरवयुक्त छंद तथा शैली में आगे बढ़ाते
हैं।’’ अस्तु अन्यत्र अनुपल्भ धृतराष्ट्र के चरित्र का
स्वतंत्र विकास ही प्रस्तुत उपन्यास की वर्ण्य-वस्तु है। भीम की
लौह-मूर्ति का अपनी भुजाओं से भंजन करने वाले वृद्ध धृतराष्ट्र के असीम बल
संचय करने की कथा उपन्यास का प्रस्थान बिंदु है।
सत्ता के समीप या उससे संलग्न नेत्रहीन व्यक्ति की संवेदनाओं, मनोभावों, आवेगों का प्रकटीकरण, सामाजिक –राजनीतिक स्थितियों के संबंध में उसकी क्रिया प्रतिक्रिया और विषम समस्याओं के प्रति उसके मनोमंथ का खुलासा उपन्यास का मुख्य प्रतिपाद्य है। अपनी आत्मकथा में धृतराष्ट्र अपने मन की परतें उघाड़ते चलते हैं। भाग्यवादी होने और सत्ता को ही सर्वस्व समझने के कारण वे किसी महानता के शिखर पर नहीं पहुँच पाते। इस कारण वे हमें एक आधुनिक पात्र-से लगते हैं।
उपन्यास के मिथकीय प्रसंगों को तर्कसम्मत रूप दिया गया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा से अलंकृत भाषा अपने लालित्य, संवेदन और प्रवाह से पाठक को तत्कालीन परिवेश में ले जाती है। कई वर्षों के शोध-अनुसंधान पर आधारित श्री सुधीर निगम की यह अभिनव कृति अब पाठकों के हाथ में है।
सत्ता के समीप या उससे संलग्न नेत्रहीन व्यक्ति की संवेदनाओं, मनोभावों, आवेगों का प्रकटीकरण, सामाजिक –राजनीतिक स्थितियों के संबंध में उसकी क्रिया प्रतिक्रिया और विषम समस्याओं के प्रति उसके मनोमंथ का खुलासा उपन्यास का मुख्य प्रतिपाद्य है। अपनी आत्मकथा में धृतराष्ट्र अपने मन की परतें उघाड़ते चलते हैं। भाग्यवादी होने और सत्ता को ही सर्वस्व समझने के कारण वे किसी महानता के शिखर पर नहीं पहुँच पाते। इस कारण वे हमें एक आधुनिक पात्र-से लगते हैं।
उपन्यास के मिथकीय प्रसंगों को तर्कसम्मत रूप दिया गया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा से अलंकृत भाषा अपने लालित्य, संवेदन और प्रवाह से पाठक को तत्कालीन परिवेश में ले जाती है। कई वर्षों के शोध-अनुसंधान पर आधारित श्री सुधीर निगम की यह अभिनव कृति अब पाठकों के हाथ में है।
भूमिका
मान्यता है कि महर्षि व्यासदेव का ग्रंथ ‘महाभारत’
आधुनिक
अर्थों में इतिहास की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसमें घटना के तिथि
क्रम और अपेक्षित आँकड़ों का अभाव है। परंतु जिसे आज हम इतिहास कहते हैं,
उस विधा के रूप में यह नितांत भिन्न प्रकृति का भी नहीं है। एक दृष्टि से
‘महाभारत’ को काव्य-विद्या में प्रस्तुत
‘अलंकृत
इतिहास’ कहा जा सकता है। इसे शुद्ध इतिहास बनाने के लिए
विद्वानों
ने कई सुझाव दिए हैं। उनके अनुसार यदि इसमें अनुस्यूत परवर्ती
आख्यान-उपाख्यान निकाल दिए जाएँ तो यह शुद्ध इतिहास हो जाएगा। इस प्रकार
का नीरस ग्रंथ ‘महाभारत’ के रूप में प्रणीत या संकलित
किया
गया होता तो यह 3000 से अधिक वर्षों तक कदापि जीवित नहीं रहता। यह तो चारण
परंपरा से प्रसूत भारतीय उपाख्यानों का कल्पवृक्ष है, एक भावात्मक कृति है
और विश्वकोश है भारतीय धर्म का—ऐसे धर्म को जो न्यूनाधित हमारे
युग
के वैज्ञानिक स्वभाव को संतुष्ट करता है, सामाजिक आकांक्षाओं के साथ
सहानुभूति रखता है, विश्व-बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त करता है।
आधुनिक पाठक को ‘महाभारत’ के जो वर्णन अविश्वसनीय लगते हैं उन पर काल के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति भी विश्वास करते थे। क्या उन बातों की कल्पना की उड़ान कहकर परित्यक्त किया जा सकता है ? ‘महाभारत’ में वर्णित वस्तुओं, मनुष्यों, पशुओं आदि की संख्याओं के संबंध में भी अक्सर विवाद उठाया जाता है। ध्यातव्य है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में संख्यावादी शब्दों की अतिशयोक्ति है। जैसे, ‘महाभारत’ के अनुसार युद्ध में एक सौ छियासठ करोड़ बीस हजार सैनिक मारे गए थे, इस पर भी मानव जाति निःशेष नहीं हुई ! कुरुक्षेत्र-युद्ध के समय सारी पृथ्वी की इतनी
जनसंख्या होने में संदेह है। वास्तव में ऐसी अतिरंजना से वर्ण्य विषय की विशालता, विविधता, विस्मयता, भयावहता, संकुलता आदि की भाव-सर्जना अभिप्रेत होती है। अतः इस विषय में चिंताकुल या आलोचनोद्यत होना निष्प्रयोजन है।
महर्षि व्यास ने अपने ग्रंथ में राजनीतिक और बौद्धिक संधान करते हुए पांडवों के चरित्र के प्रत्येक शुभ पक्ष का विशद वर्णन किया है। कथा–प्रवाह को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए घटनाओं के मोड़ पर कौरव-पात्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है जिससे वे सर्वत्र खल-पात्र के रूप में दिखाई दें। इस हेतु ग्रंथाकार को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सज्जन और दुर्जन का, सत्य और असत्य का, परार्थ और स्वार्थ का, शांति और संघर्ष का द्वंद्व दैवीय विधान माना जाता है।
व्यास ने उसी परंपरा का पालन किया है। द्वापर का युग आज के लिए समीचीन है क्योंकि वर्तमान युग में भी वैसा ही पारस्परिक संघर्ष है, छल है, वैसी ही प्रतिशोधी भावना है, मनोहतता है, निराशा है, संतति-मोह है, सत्ता लोलुपता है और सर्वोपरि मूल्यहीनता है। आज भी युद्ध-महायुद्ध होते हैं और हिंसा से राष्ट्रों के मन चूर-चूर होते हैं।
मनुष्यों के हृदय में दुष्टता, स्वार्थ और द्वेष की पंकिल धारा प्रवाहित होती है, जिसे बाँधने में हमारी जीवन-प्रणाली अक्षम सिद्ध हुई है।
मनुष्य ऐतिहासिक प्राणी है। वह अतीत की सांस्कृति समृद्धियों को आत्मसात् करके विकास की ओर अग्रसर होता है। आत्मसात करने की क्षमता उसकी सजीव कल्पना और प्रयोजनीय कर्तृत्व-शक्ति पर निर्भर करती है। इस हेतु प्राचीन इतिहास की पुनर्व्याख्या और उसकी नवीकरण परंपरित व्यवस्था की संरचना को, विकासशील राष्ट्र के रूप को, व्यक्ति की जीवन-पद्धति को नया आयाम देते हैं।
प्रस्तुत कृति ‘मैं धृतराष्ट्र के केंद्रीय पात्र धृतराष्ट्र हैं। वे किसी महानता के शिखर पर पहुँचे हुए व्यक्ति नहीं है। हम उन्हें यात्रा की निरन्तरता में पाते हैं। धृतराष्ट्र को सर्वांग रूप से समझने के लिए उन्हें अपनी कथा स्वयं कहने की स्वतंत्रता इस शर्त पर दी गई है कि वे अपने मन का मोह, कलुष, विकार, संदेह, धृष्टता तक हमसे गोपन नहीं रखेंगे और अपनी असफलताओं के माध्यम से पाठकों के समक्ष पहुँचेंगे। धृतराष्ट्र की कथा तब से प्रारंभ होती है जब वे इसे कहने के योग्य हो जाते हैं।
पांडु और धृत के बाल्यकाल से युवावस्था तक के संबंधों का चित्रण करने के लिए कई काल्पनिक पात्रों और घटनाओं का प्रश्रय लिया गया है। प्रारंभ से ही अंध धृतराष्ट्र एक उत्साही बालक हैं, प्रेमिल अग्रज है, जिज्ञासु शिष्य हैं। नेत्रहीन बालकों की शिक्षा देने की समस्या, आज की अपेक्षा उस काल में अधिक जटिल थी। धृत राजपुत्र हैं अतः उस एक विद्यार्थी के लिए एक योग्य गुरु नियुक्त किया जाता है। गुरु अपने शिष्य की मानसिक और शारीरिक शक्तियों का विकास तो करते हैं साथ ही उसकी श्रव्य और प्राण शक्तियों को भी अनुपस्थित दृष्टि-क्षमता का स्थानापन्न बना देते हैं।
इस हेतु वे प्राकृतिक उपादानों और साधनों का प्रश्रय लेते हैं। ‘महाभारत’ में एक प्रसंग हैं कि युद्ध समाप्ति के पश्चात युद्ध-भूमि में ही पाँचों पांडव धृतराष्ट्र से भेंट करते हैं। सर्वप्रथम युधिष्ठिर उनके कंठ से लगते हैं। भीम की बारी आने पर उसके स्थान पर एक लौहमूर्ति धृतराष्ट्र के सम्मुख कर दी जाती है, जिसे वे भीम समझकर, अलिंगनबद्ध कर, अपने बाहुबल से भंजित कर देते हैं। यह प्रसंग भले ही अतिरंजित हो, काल्पनिक हो या प्रक्षिप्त हो,
यह सूचना तो देता ही है कि लोक में धृतराष्ट्र को अत्यंत बलशाली माना जाता था। गुरु के सान्निध्य में ऐसा ही बल संचित करके दृष्टिगत होते हैं।
धृत और पांडु का प्रेम इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रकृत है कि अनुज होने के कारण पांडु अपना राज्याभिषेक कराने से मना कर देते हैं। अग्रज के आदेश से ही वे राज-पद स्वीकार करते हैं और पूरा राजकाज उनके मार्गदर्शन में चलाते हैं। पांडु के वन-प्रवास की अवधि में भी दोनों भ्राताओं के सौहार्दपूर्ण संबंध तब तक बने रहते हैं जब तक पाडु व्यावहारिक कारणों से, अग्रज से और राज्य से अपने संबंध समाप्त नहीं कर देते।
धृतराष्ट्र के निष्पाप मनोभूमि पर ईर्ष्या के विष-बीज का प्रथम वपन, अपनी भगिनी का परिणय कराने आए गंधार राजकुमार शकुनि ने किया था। कालांतर में यही बीज पुत्र-मोह की खाद पाकर, अबाधित सत्ता-भोग के ईहा-जल से सिंचित होकर और गण समाज में राज सभा की ह्रासमान शक्ति से प्राण-वायु पाकर महावृक्ष के रूप में पल्लवित-पुष्पित होता चला गया। अपराजेय कर्मशक्ति के प्रतीक कृष्ण भी अपने अमृत वचनों से इस विष-वृक्ष को निर्वषित नहीं कर पाए। इस वृक्ष की छाया तले शरण पाए व्यक्तियों में इंद्रिय-बोध है, संवेदनाएँ हैं, भावनाएँ हैं, परंतु आत्मा सुप्त होकर अनुपस्थित है। कभी-कभार बाह्य प्रभाव से एक क्षीण प्रकाश-रेखा उदित होती है और आत्मा को जाग्रत कर, उससे किंचित सत्कर्म कराके पुनः लुप्त हो जाती है।
धृतराष्ट्र स्थायी रूप से सहज स्नेह-वृत्त में किसी से नहीं जुड़ पाते—न पुत्र से, न पत्नी से, न विदुर-सम मंत्री से। उनका आत्म-प्रेम अन्य सभी संबंधों के ऊपर ध्वनित होता है। दौत्य कार्य के लिए प्रस्तुत संजय से वे एकांत में कहते हैं कि वह पांडवों के समक्ष उनकी अपनी छवि निर्दोष प्रतिपादित करें और दुर्योधन को शाति-स्थापना के मार्ग में अवरोधक सिद्ध करे। कौरव सभा में शातिदूत कृष्ण के समक्ष दुर्योधन को बुलाकर गांधारी द्वारा समझाने और सुमार्ग पर लाने का पूरा श्रेय वे पत्नी को नहीं देना चाहते। पांडवों की पक्षधरता के कारण वे विदुर को हस्तिनापुर से निष्कासित कर दते हैं और
भातृ-प्रेम के नाम पर तभी वापस बुलाते हैं जब उन्हें विदुर का पांडवों के पक्ष में चले जाने का भय सताता है। धृतराष्ट्र का आचरण सहज न होकर स्वार्थ-बुद्धि से परिचालित होता है, इसी कारण पग-पग पर उनका अन्यथाचरण देखने को मिलता है। इससे वे मानवीय व्यवहार की जटिल भूमिका में उतरते चले गए हैं। वत्सल पिता की निर्मम नियति ढोते इस पात्र को इतनी स्वतंत्रता अवश्य दी गई है कि वह अपने अंतर्द्वंद्वों की, मनस्ताप की अभिव्यक्ति करता चले ताकि कथा आगे बढ़ाने के लिए वह स्वयं को निर्भार अनुभव करे।
उपन्यास के कथ्य पर नैतिकता का आवरण नहीं डाला गया है। तत्समय अवसन्न गण-समाज के दोषों-क्रूरता और हिंसा का व्यापक चलन, युवा स्त्रियों का राजमहल में दासीत्व, रति-स्वातंत्र्य, कन्याहरण, स्वयंवर, नियोग, प्रतिहिंसा के भाव के शमितार्थ अनियंत्रित क्रूरता-प्रदर्शन का यथातथ्य किंतु शालीन वर्णन किया गया है।
‘मैं धृतराष्ट्र’ में अविश्वसनीय स्थितियों से या तो बचा गया है या अपेक्षित होने पर उनका वैज्ञानिक-धरातल पर चित्रण किया गया है। माना जाता है कि धृतराष्ट्र के अंधत्व का कारण उनकी माता द्वारा नियोग के समय अपनी आँखों पर हाथ रख लेना था। इस परवर्ती अवैज्ञानिक धारणा को विवेक-सम्मत आधार दिया गया है। बहुचर्चित द्रौपदी चीरहरण प्रसंग मूल महाभारत में नहीं है, अतः इससे बचा गया है तथापि दुर्योधन-मंडल का दुराचरण यथावत् रहा है। गांधारी के सौ पुत्रों के जन्म की कथा भी विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत की गई है।
कृष्ण और भीष्म की तरह विदुर भी प्राचीन दर्शन ‘प्रज्ञावाद’ के पोषक थे। इसे वे अध्यात्म और ईश्वर से संबंद्ध कर देखते थे। धृतराष्ट्र के भाग्यवाद और विदुर के प्रज्ञावाद के निरूपण को किंचित विस्तार दिया गया है ताकि पाठक सहज ही अनुभूत कर लें कि धृतराष्ट्र की अवस्था कर्म और पुरुषार्थ में नहीं है। ‘जो जैसा है वह निर्विघ्न वैसा ही बना रहे’—यहीं तक उनके विचार की दौड़ थी। धृतराष्ट्र के अपने मिथक हैं, वे उनसे आक्रांत होने के कारण तर्क की ओर संक्रमण नहीं कर पाते।
महाभारत-युद्ध के समय ऋषभ संप्रदाय (जो कालांतर में जैन धर्म के नाम से विख्यात हुआ) के तीर्थकर आचार्य नेमिनाथ विद्यमान थे, परंतु ‘महाभारत’ में उनका उल्लेख नहीं है। यह बात अविश्वसनीय लगती है कि अहिंसा के पुजारी को आसन्न युद्ध-जन्य घोर हिंसा की सूचना मिले और वे किसी युद्धकामी पक्ष से मिलकर उसे युद्ध से विरत करने की चेष्टा न करें। कथांतर की स्वतंत्रता लेते हुए उपन्यास में आचार्य नेमिनाथ और युधिष्ठिर की संक्षिप्त भेंट दिखाई गई है। आचार्यवर ने अपना मत रखा परंतु क्षत्रिय रूपी चट्टान पर अहिंसा की कोमल दूब उगाई न जा सकी। उन्होंने जोर भी नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वे अपने विचार किसी पर थोपना भी एक प्रकार की हिंसा ही है।
अंत में धृतराष्ट्र वन-गमन करते हैं। उन्हें मोक्ष की आकाक्षा है परन्तु संन्यास की ओर वे सात्त्विक भाव से प्रवृत्त नहीं हुए हैं। पांडवों के साथ रहते हुए ऐसे जटिलताएँ उत्पन्न हो गई थीं, जिनसे आक्रांत हो उन्हें पारिवारिक परिवेश से पलायन करना पड़ा। भीम उनके हृदय में गँसी ऐसी फांस है, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व के संवेदनशील भाग पर उपेक्षा की धूल जमने लगती है। पीछे देखने के लिए उनके पास कोई महान अतीत नहीं है
अतः अपना दारुण वर्तमान लेकर, एक निर्लिप्त भविष्य की खोज में वे वन-गमन करते हैं। जाने से पूर्व वे जनता के समक्ष अपने कुशासन और भूलों के लिए तथा दुर्योधन के कृत-अपराधों के लिए हार्दिक क्षमायाचना करते हैं, मार्मिक पश्चाताप करते हैं। धृतराष्ट्र अंत समय तक अपनी कथा कहते रहते हैं। मृत्यु से पूर्व उनके मुख से ‘शुभम्’ शब्द निस्रत होता है। इसी के साथ उपन्यास विश्राम लेता है।
यह संक्षिप्त भूमिका न तो उपन्यास का सार-संक्षेप है और न ही प्रचलित महाभारत-कथा के विचलन बिंदुओं का स्पष्टीकरण है। पूरे उपन्यास में धृतराष्ट्र ने लेखक को बोलने का कोई अवसर नहीं दिया है। इसलिए लेखक को अपने मनोभाव प्रकट करने के लिए भूमिका का प्रक्षय लेना पड़ा।
इस उपन्यास के प्रणयन में मुझे दो से अधिक वर्षों का समय लगा। यद्यपि व्यासदेव का ‘महाभारत’ ही इसका उपजीव्य ग्रंथ है, परंतु मैंने अन्य अनेक ग्रंथों, पुस्तकों, आलेखों की सहायता ली है। श्री वासुदेवशरण अग्रवाल के ग्रंथ ‘भारत-सावित्री’ (3 खंड) से मुझे मूल महाभारत की पहचान करने तथा दर्शन के गूढ़ विषयों को समझने में सहायता मिली है। मैं तथा अन्य विद्वान् लेखकों के प्रति अपने श्रृद्धा-सुमन अर्पित करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। मेरी पुत्रियों श्वेता और अंजलि ने मूल पाठ-लेखन, कंप्यूटर-टंकण, प्रूफ-शोधन में सहायता दी है। इस हेतु मैं उन्हें स्नेहाशीष देता हूँ। मुझे गार्हस्थ्यिक उत्तर- दायित्वों से मुक्ति देकर और मेरे स्वास्थ्य का अनवरत अनुरक्षण करके मेरी धर्मपत्नी सुमन ने उपन्यास-लेखन में जो अमूल्य प्रच्छन सहयोग दिया है, उसके अभाव में यह उपन्यास कब पूर्ण कर पाता या कर भी पाता अथवा नहीं, मैं नहीं जानता। पत्नी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में यह कृति मैं उन्हें सप्रेम समर्पित करता हूँ।
आधुनिक पाठक को ‘महाभारत’ के जो वर्णन अविश्वसनीय लगते हैं उन पर काल के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति भी विश्वास करते थे। क्या उन बातों की कल्पना की उड़ान कहकर परित्यक्त किया जा सकता है ? ‘महाभारत’ में वर्णित वस्तुओं, मनुष्यों, पशुओं आदि की संख्याओं के संबंध में भी अक्सर विवाद उठाया जाता है। ध्यातव्य है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में संख्यावादी शब्दों की अतिशयोक्ति है। जैसे, ‘महाभारत’ के अनुसार युद्ध में एक सौ छियासठ करोड़ बीस हजार सैनिक मारे गए थे, इस पर भी मानव जाति निःशेष नहीं हुई ! कुरुक्षेत्र-युद्ध के समय सारी पृथ्वी की इतनी
जनसंख्या होने में संदेह है। वास्तव में ऐसी अतिरंजना से वर्ण्य विषय की विशालता, विविधता, विस्मयता, भयावहता, संकुलता आदि की भाव-सर्जना अभिप्रेत होती है। अतः इस विषय में चिंताकुल या आलोचनोद्यत होना निष्प्रयोजन है।
महर्षि व्यास ने अपने ग्रंथ में राजनीतिक और बौद्धिक संधान करते हुए पांडवों के चरित्र के प्रत्येक शुभ पक्ष का विशद वर्णन किया है। कथा–प्रवाह को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए घटनाओं के मोड़ पर कौरव-पात्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है जिससे वे सर्वत्र खल-पात्र के रूप में दिखाई दें। इस हेतु ग्रंथाकार को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सज्जन और दुर्जन का, सत्य और असत्य का, परार्थ और स्वार्थ का, शांति और संघर्ष का द्वंद्व दैवीय विधान माना जाता है।
व्यास ने उसी परंपरा का पालन किया है। द्वापर का युग आज के लिए समीचीन है क्योंकि वर्तमान युग में भी वैसा ही पारस्परिक संघर्ष है, छल है, वैसी ही प्रतिशोधी भावना है, मनोहतता है, निराशा है, संतति-मोह है, सत्ता लोलुपता है और सर्वोपरि मूल्यहीनता है। आज भी युद्ध-महायुद्ध होते हैं और हिंसा से राष्ट्रों के मन चूर-चूर होते हैं।
मनुष्यों के हृदय में दुष्टता, स्वार्थ और द्वेष की पंकिल धारा प्रवाहित होती है, जिसे बाँधने में हमारी जीवन-प्रणाली अक्षम सिद्ध हुई है।
मनुष्य ऐतिहासिक प्राणी है। वह अतीत की सांस्कृति समृद्धियों को आत्मसात् करके विकास की ओर अग्रसर होता है। आत्मसात करने की क्षमता उसकी सजीव कल्पना और प्रयोजनीय कर्तृत्व-शक्ति पर निर्भर करती है। इस हेतु प्राचीन इतिहास की पुनर्व्याख्या और उसकी नवीकरण परंपरित व्यवस्था की संरचना को, विकासशील राष्ट्र के रूप को, व्यक्ति की जीवन-पद्धति को नया आयाम देते हैं।
प्रस्तुत कृति ‘मैं धृतराष्ट्र के केंद्रीय पात्र धृतराष्ट्र हैं। वे किसी महानता के शिखर पर पहुँचे हुए व्यक्ति नहीं है। हम उन्हें यात्रा की निरन्तरता में पाते हैं। धृतराष्ट्र को सर्वांग रूप से समझने के लिए उन्हें अपनी कथा स्वयं कहने की स्वतंत्रता इस शर्त पर दी गई है कि वे अपने मन का मोह, कलुष, विकार, संदेह, धृष्टता तक हमसे गोपन नहीं रखेंगे और अपनी असफलताओं के माध्यम से पाठकों के समक्ष पहुँचेंगे। धृतराष्ट्र की कथा तब से प्रारंभ होती है जब वे इसे कहने के योग्य हो जाते हैं।
पांडु और धृत के बाल्यकाल से युवावस्था तक के संबंधों का चित्रण करने के लिए कई काल्पनिक पात्रों और घटनाओं का प्रश्रय लिया गया है। प्रारंभ से ही अंध धृतराष्ट्र एक उत्साही बालक हैं, प्रेमिल अग्रज है, जिज्ञासु शिष्य हैं। नेत्रहीन बालकों की शिक्षा देने की समस्या, आज की अपेक्षा उस काल में अधिक जटिल थी। धृत राजपुत्र हैं अतः उस एक विद्यार्थी के लिए एक योग्य गुरु नियुक्त किया जाता है। गुरु अपने शिष्य की मानसिक और शारीरिक शक्तियों का विकास तो करते हैं साथ ही उसकी श्रव्य और प्राण शक्तियों को भी अनुपस्थित दृष्टि-क्षमता का स्थानापन्न बना देते हैं।
इस हेतु वे प्राकृतिक उपादानों और साधनों का प्रश्रय लेते हैं। ‘महाभारत’ में एक प्रसंग हैं कि युद्ध समाप्ति के पश्चात युद्ध-भूमि में ही पाँचों पांडव धृतराष्ट्र से भेंट करते हैं। सर्वप्रथम युधिष्ठिर उनके कंठ से लगते हैं। भीम की बारी आने पर उसके स्थान पर एक लौहमूर्ति धृतराष्ट्र के सम्मुख कर दी जाती है, जिसे वे भीम समझकर, अलिंगनबद्ध कर, अपने बाहुबल से भंजित कर देते हैं। यह प्रसंग भले ही अतिरंजित हो, काल्पनिक हो या प्रक्षिप्त हो,
यह सूचना तो देता ही है कि लोक में धृतराष्ट्र को अत्यंत बलशाली माना जाता था। गुरु के सान्निध्य में ऐसा ही बल संचित करके दृष्टिगत होते हैं।
धृत और पांडु का प्रेम इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रकृत है कि अनुज होने के कारण पांडु अपना राज्याभिषेक कराने से मना कर देते हैं। अग्रज के आदेश से ही वे राज-पद स्वीकार करते हैं और पूरा राजकाज उनके मार्गदर्शन में चलाते हैं। पांडु के वन-प्रवास की अवधि में भी दोनों भ्राताओं के सौहार्दपूर्ण संबंध तब तक बने रहते हैं जब तक पाडु व्यावहारिक कारणों से, अग्रज से और राज्य से अपने संबंध समाप्त नहीं कर देते।
धृतराष्ट्र के निष्पाप मनोभूमि पर ईर्ष्या के विष-बीज का प्रथम वपन, अपनी भगिनी का परिणय कराने आए गंधार राजकुमार शकुनि ने किया था। कालांतर में यही बीज पुत्र-मोह की खाद पाकर, अबाधित सत्ता-भोग के ईहा-जल से सिंचित होकर और गण समाज में राज सभा की ह्रासमान शक्ति से प्राण-वायु पाकर महावृक्ष के रूप में पल्लवित-पुष्पित होता चला गया। अपराजेय कर्मशक्ति के प्रतीक कृष्ण भी अपने अमृत वचनों से इस विष-वृक्ष को निर्वषित नहीं कर पाए। इस वृक्ष की छाया तले शरण पाए व्यक्तियों में इंद्रिय-बोध है, संवेदनाएँ हैं, भावनाएँ हैं, परंतु आत्मा सुप्त होकर अनुपस्थित है। कभी-कभार बाह्य प्रभाव से एक क्षीण प्रकाश-रेखा उदित होती है और आत्मा को जाग्रत कर, उससे किंचित सत्कर्म कराके पुनः लुप्त हो जाती है।
धृतराष्ट्र स्थायी रूप से सहज स्नेह-वृत्त में किसी से नहीं जुड़ पाते—न पुत्र से, न पत्नी से, न विदुर-सम मंत्री से। उनका आत्म-प्रेम अन्य सभी संबंधों के ऊपर ध्वनित होता है। दौत्य कार्य के लिए प्रस्तुत संजय से वे एकांत में कहते हैं कि वह पांडवों के समक्ष उनकी अपनी छवि निर्दोष प्रतिपादित करें और दुर्योधन को शाति-स्थापना के मार्ग में अवरोधक सिद्ध करे। कौरव सभा में शातिदूत कृष्ण के समक्ष दुर्योधन को बुलाकर गांधारी द्वारा समझाने और सुमार्ग पर लाने का पूरा श्रेय वे पत्नी को नहीं देना चाहते। पांडवों की पक्षधरता के कारण वे विदुर को हस्तिनापुर से निष्कासित कर दते हैं और
भातृ-प्रेम के नाम पर तभी वापस बुलाते हैं जब उन्हें विदुर का पांडवों के पक्ष में चले जाने का भय सताता है। धृतराष्ट्र का आचरण सहज न होकर स्वार्थ-बुद्धि से परिचालित होता है, इसी कारण पग-पग पर उनका अन्यथाचरण देखने को मिलता है। इससे वे मानवीय व्यवहार की जटिल भूमिका में उतरते चले गए हैं। वत्सल पिता की निर्मम नियति ढोते इस पात्र को इतनी स्वतंत्रता अवश्य दी गई है कि वह अपने अंतर्द्वंद्वों की, मनस्ताप की अभिव्यक्ति करता चले ताकि कथा आगे बढ़ाने के लिए वह स्वयं को निर्भार अनुभव करे।
उपन्यास के कथ्य पर नैतिकता का आवरण नहीं डाला गया है। तत्समय अवसन्न गण-समाज के दोषों-क्रूरता और हिंसा का व्यापक चलन, युवा स्त्रियों का राजमहल में दासीत्व, रति-स्वातंत्र्य, कन्याहरण, स्वयंवर, नियोग, प्रतिहिंसा के भाव के शमितार्थ अनियंत्रित क्रूरता-प्रदर्शन का यथातथ्य किंतु शालीन वर्णन किया गया है।
‘मैं धृतराष्ट्र’ में अविश्वसनीय स्थितियों से या तो बचा गया है या अपेक्षित होने पर उनका वैज्ञानिक-धरातल पर चित्रण किया गया है। माना जाता है कि धृतराष्ट्र के अंधत्व का कारण उनकी माता द्वारा नियोग के समय अपनी आँखों पर हाथ रख लेना था। इस परवर्ती अवैज्ञानिक धारणा को विवेक-सम्मत आधार दिया गया है। बहुचर्चित द्रौपदी चीरहरण प्रसंग मूल महाभारत में नहीं है, अतः इससे बचा गया है तथापि दुर्योधन-मंडल का दुराचरण यथावत् रहा है। गांधारी के सौ पुत्रों के जन्म की कथा भी विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत की गई है।
कृष्ण और भीष्म की तरह विदुर भी प्राचीन दर्शन ‘प्रज्ञावाद’ के पोषक थे। इसे वे अध्यात्म और ईश्वर से संबंद्ध कर देखते थे। धृतराष्ट्र के भाग्यवाद और विदुर के प्रज्ञावाद के निरूपण को किंचित विस्तार दिया गया है ताकि पाठक सहज ही अनुभूत कर लें कि धृतराष्ट्र की अवस्था कर्म और पुरुषार्थ में नहीं है। ‘जो जैसा है वह निर्विघ्न वैसा ही बना रहे’—यहीं तक उनके विचार की दौड़ थी। धृतराष्ट्र के अपने मिथक हैं, वे उनसे आक्रांत होने के कारण तर्क की ओर संक्रमण नहीं कर पाते।
महाभारत-युद्ध के समय ऋषभ संप्रदाय (जो कालांतर में जैन धर्म के नाम से विख्यात हुआ) के तीर्थकर आचार्य नेमिनाथ विद्यमान थे, परंतु ‘महाभारत’ में उनका उल्लेख नहीं है। यह बात अविश्वसनीय लगती है कि अहिंसा के पुजारी को आसन्न युद्ध-जन्य घोर हिंसा की सूचना मिले और वे किसी युद्धकामी पक्ष से मिलकर उसे युद्ध से विरत करने की चेष्टा न करें। कथांतर की स्वतंत्रता लेते हुए उपन्यास में आचार्य नेमिनाथ और युधिष्ठिर की संक्षिप्त भेंट दिखाई गई है। आचार्यवर ने अपना मत रखा परंतु क्षत्रिय रूपी चट्टान पर अहिंसा की कोमल दूब उगाई न जा सकी। उन्होंने जोर भी नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वे अपने विचार किसी पर थोपना भी एक प्रकार की हिंसा ही है।
अंत में धृतराष्ट्र वन-गमन करते हैं। उन्हें मोक्ष की आकाक्षा है परन्तु संन्यास की ओर वे सात्त्विक भाव से प्रवृत्त नहीं हुए हैं। पांडवों के साथ रहते हुए ऐसे जटिलताएँ उत्पन्न हो गई थीं, जिनसे आक्रांत हो उन्हें पारिवारिक परिवेश से पलायन करना पड़ा। भीम उनके हृदय में गँसी ऐसी फांस है, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व के संवेदनशील भाग पर उपेक्षा की धूल जमने लगती है। पीछे देखने के लिए उनके पास कोई महान अतीत नहीं है
अतः अपना दारुण वर्तमान लेकर, एक निर्लिप्त भविष्य की खोज में वे वन-गमन करते हैं। जाने से पूर्व वे जनता के समक्ष अपने कुशासन और भूलों के लिए तथा दुर्योधन के कृत-अपराधों के लिए हार्दिक क्षमायाचना करते हैं, मार्मिक पश्चाताप करते हैं। धृतराष्ट्र अंत समय तक अपनी कथा कहते रहते हैं। मृत्यु से पूर्व उनके मुख से ‘शुभम्’ शब्द निस्रत होता है। इसी के साथ उपन्यास विश्राम लेता है।
यह संक्षिप्त भूमिका न तो उपन्यास का सार-संक्षेप है और न ही प्रचलित महाभारत-कथा के विचलन बिंदुओं का स्पष्टीकरण है। पूरे उपन्यास में धृतराष्ट्र ने लेखक को बोलने का कोई अवसर नहीं दिया है। इसलिए लेखक को अपने मनोभाव प्रकट करने के लिए भूमिका का प्रक्षय लेना पड़ा।
इस उपन्यास के प्रणयन में मुझे दो से अधिक वर्षों का समय लगा। यद्यपि व्यासदेव का ‘महाभारत’ ही इसका उपजीव्य ग्रंथ है, परंतु मैंने अन्य अनेक ग्रंथों, पुस्तकों, आलेखों की सहायता ली है। श्री वासुदेवशरण अग्रवाल के ग्रंथ ‘भारत-सावित्री’ (3 खंड) से मुझे मूल महाभारत की पहचान करने तथा दर्शन के गूढ़ विषयों को समझने में सहायता मिली है। मैं तथा अन्य विद्वान् लेखकों के प्रति अपने श्रृद्धा-सुमन अर्पित करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। मेरी पुत्रियों श्वेता और अंजलि ने मूल पाठ-लेखन, कंप्यूटर-टंकण, प्रूफ-शोधन में सहायता दी है। इस हेतु मैं उन्हें स्नेहाशीष देता हूँ। मुझे गार्हस्थ्यिक उत्तर- दायित्वों से मुक्ति देकर और मेरे स्वास्थ्य का अनवरत अनुरक्षण करके मेरी धर्मपत्नी सुमन ने उपन्यास-लेखन में जो अमूल्य प्रच्छन सहयोग दिया है, उसके अभाव में यह उपन्यास कब पूर्ण कर पाता या कर भी पाता अथवा नहीं, मैं नहीं जानता। पत्नी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में यह कृति मैं उन्हें सप्रेम समर्पित करता हूँ।
-सुधीर निगम
धृतराष्ट्र का प्रतिवेदन
हजारों वर्ष लाँघकर मैं हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र अपनी गाथा सुनाने
बैठा हूँ। कुछ लोगों को यह आपत्ति हो सकती है कि मेरी गाथा क्यों सुनी
जाए, मैं तो महाभारत का कृष्ण-पक्ष हूँ, असत्य का प्रतिरूप हूँ,
कुसंस्कार, दुःस्वप्न, आतंक, तमिस्रा का रूप हूँ जिस पर सत्यरूपी पांडवों
की विजय हुई थी। परन्तु यह विजय अस्थाई सिद्ध हुई क्योंकि असत्य एक
प्रवृत्ति होने के कारण आज भी जीवित है।
मेरे पुत्रों और पांडु-पुत्रों के मध्य वंश विभाजन की रेखा खींचना सरल नहीं है। पांडु-पुत्रों को पांडव तो कहा जा सकता है पर कौरव के वजन पर क्यों नहीं क्योंकि हमसे पंद्रहवीं पीढ़ी पूर्व हमारे वंश में कुरु नामक राजा हुए थे और उन्हीं के नाम पर कौरव वंश चला। अतः जैसे पांडु-पुत्रों का पितृवाचक नाम पांडव है वैसे ही मेरे पुत्रों का नाम ‘धार्तराष्ट्र’ हुआ। यह नाम अक्सर नहीं लिया जाता। इतिहास की जो वक्र रेखाएं हैं उन्हें सरल करना है मेरा ध्येय है।
मेरे जनक व्यासदेव ने मेरे साथ पूर्ण न्याय नहीं किया। कहा जाता है कि पिता के लिए दो पुत्र दोनों आँखों के समान होते हैं। पर कौन जानता है कि दोनों आँखों की दृश्य-शक्ति अक्सर बराबर नहीं होती उनकी भावनाओं का पलड़ा सदैव पांडु और उसके बाद उनके पुत्रों की ओर झुका रहा। जब संघर्ष की स्थिति आई तो वे उनके साथ खड़े दिखाई दिए। हमारा चित्र स्वयं धुंधला होता चला गया। यहाँ हमने विदुर की बात नहीं कही है। यथास्थान उनके प्रति हुए अन्याय की गाथा भी आपको सुनाऊँगा।
मैं और पांडु व्यास जी के क्षेत्रज पुत्र थे। उन्होंने न हमारा शैशव देखा, न कैशोर्य और न ही यौवन का प्रथम चरण। वे अपनी साधना में लीन रहे, अतः हमारी यह गाथा अपने ग्रंथ में समाहित नहीं कर सके। मेरा और पाडु का बचपन विस्मृति के गर्त में समाया है। मैं इसे बाहर लाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा।
कथा कहने की जो विधा आज प्रचलित है मेरा ढंग उससे भिन्न होगा। भई, मैं 3-4 हजार वर्ष पुराना जो हूँ। तत्समय पिता की या किसी अग्रज की उसी के मुख पर आलोचना करना अशिष्ट नहीं माना जाता था। दुर्योधन जब मेरी या विदुर की भर्त्सना करने लगे तो उसे कम से कम इस कारण अशिष्ट या धृष्ट नहीं समझना चाहिए मैं भी अपने जनक, जननी या पत्नी के प्रति असहिष्णु हो उठूँ तो मुझे क्षमा करते रहिएगा क्योंकि मेरी गाथा जड़ उपाख्यान नहीं है
प्रत्युत मानव जीवन में चिरकाल से प्रवाहमान धारा है। आप आधुनिक हैं अतः हमारी अनेक बातें आपको अविश्वसनीय लग सकती हैं। परंतु उन बातों पर उस काल के सर्वाधिक ज्ञानी व्यक्ति भी विश्वास करते थे क्योंकि वे ज्ञान से विज्ञान और ऊपर उठकर प्रज्ञान—स्वंय सहित संपूर्ण जीवन का अपने अंदर चेतन ज्ञान-तक पहुँच गए थे। आपका विज्ञान पूर्णता की यात्रा में है। जिस दिन चौथा आयाम ज्ञात हो जाएगा उस दिन आधुनिक जगत् समझ पाएगा कि व्यास की ‘दिव्य-दृष्टि’ क्या थी और उसे अस्थायी रूप से संजय को कैसे दिया गया; समस्त जगत् को अच्छी प्रकार से ज्यों का त्यों देखने की व्यास को प्राप्त ‘प्रतिस्मृति विद्या’ थी !
मेरी गाथा में अविश्वसनीयता के छिद्र दृष्टिगत हो सकते हैं। यह गाथा द्वापर युग की है। द्वार का अर्थ है ‘संदेह’ है। सच कहूँ तो उस समय का मानव संदेहशील हो उठा था, उसमें अविश्वास जड़ें जमाने लगा था, शारीरिक सुख की वासना प्रधान हो गई थी, भोग ही लक्ष्य बन गया था, भोग के लिए संचय प्रारंभ हो गया था, कष्ट-सहिष्मुता और त्याग का लोप हो चुका था। यह सब विकृतियाँ पल्लवित होकर आज भी तहलका मचा रही हैं, अंतर यही है कि उस समय व्यक्ति धर्मभीरु था, उसका उपार्जन पवित्र था। इसे पढ़कर ही आप समझ पाएँगे कि मैं खलरूप नहीं हूँ प्रत्युत ऐसा व्यक्ति हूँ जो अस्तित्व के अंधकार में भटकता हुआ प्रकाश के लिए पुत्ररूपी अग्निशिखा से लिपट जाता है। पुत्र-मोह मेरी जड़ता थी, देखता हूँ वैसी जड़ें आज भी उन्मीलित नहीं हो पाई हैं।
भाग्यवादी होने के कारण मैं किसी की महानता के शिखर पर नहीं पहुँच पाया। पांडु के उच्छिष्ट राज्य पर मैं रक्षक-सर्प बनकर जरूर बैठा परंतु उस पर अपने नैसर्गिक अधिकार का विष वमन करता रहा। महानता सत्ता में नहीं होती वह होती है संघर्ष में, लोक से संबंध होने में, पुरुषार्थ में, कर्म में, मुझे सत्ता मिली, मैं कर्म-च्युत हो गया—कुछ अपनी सोच के कारण शेष अपनी परिस्थितियों के वशीभूत होकर। मेरा सोच सदा यही रहा, ‘‘ब्रह्मा ने जो रच दिया है, सारा जगत् वैसी ही चेष्टा में लगा हुआ है।’
मैंने कई अवसरों पर इतिहास की अनिवार्यता को नकारा। राजा होने के नाते यदि मैं उन क्षणों को पकड़ पाता, मेरी प्रज्ञा स्थायी रहती तो मेरा काल-खंड इतिहास में श्लाघ्य होता। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मानव इतिहास में युद्ध से सर्वथा मुक्त एक भी युग नहीं दिखाई पड़ता और ऐसी पीढ़ियाँ शायद ही हों जिन्होंने संघर्ष के दर्शन न किए हों। समुद्र के नियमित ज्वार के समान ही संघर्षों की, युद्धों-महायुद्धों की तरंगे भी उठती-बैठती हैं।
परंतु मेरे जीवन में ज्वार तो आया पर उसका अवसान भाटा नहीं हुआ ! इतिहास ने सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया यदि मैंने दृढ़ इच्छा-शक्ति से काम लिया होता तो कृष्ण द्वारा प्रस्तुत संधि का अनुमोदन किया जा सकता था, युद्ध टल सकता था, कौरवों-पांडवों में सौमनस्य स्थापित हो सकता था, पांडवों को उनका राज्य वापस दिया जा सकता था। हाँ, यह सब मैं कर सकता था परंतु विवश था क्योंकि मैं वास्तविक शक्ति-केन्द्र नहीं रह गया था। मैं पांडवों को दोष नहीं देता, पर कहना पड़ेगा कि युद्ध की प्रथम भेरी उन्होंने ही बजाई। उन्होंने पहला शांतिदूत ब्राह्मण के रूप में भेजा। कृष्ण के मना करने पर भी पांडवों ने सैन्य संग्रह प्रारंभ कर दिया।
मैं नहीं जानता कि मेरा जीवन क्यों अशांत रहा, दुविधाग्रस्त रहा, शंकापूरित रहा, स्वार्थ से आवृत्त रहा, दीन बनकर जलता-कुढ़ता रहा ! पता नहीं क्यों मैं अंतर्मुखी होकर घुटन और आत्मपीड़न की अंध-गुफा में उतर जाता रहा ! पथभ्रष्ट महत्वाकांक्षाओं की चाह से संशप्त पुत्र के, या कहूँ दुर्योधन के मोह ने मुझे भीरु बना दिया, प्रज्ञांध बना दिया। पुत्र-मोह ने मेरे जीवन में अतलांत खाइयाँ पैदा कर दीं तो मैं निरपेक्षता की सम-भूमि पर कैसे चल पाता ? विदुर के नीति परक वचन भी मेरा भावांतरण नहीं कर पाए। न्याय के मार्ग पर मैं तभी चला जब मेरे शरीर में काँटे चुभे।
गांधारी की प्रेरणा से अनुप्राणित होकर मैंने कई बार धृतात्मा बनने का प्रयास किया, लोक-कल्याण की भद्र भावना ने अनुप्राणित होने की कामना की परंतु इस प्रयास या कामना के साथ फलवती चेष्टा का संयोग कभी नहीं हो पाया। खुलकर बात करने में सदा संकोच करता रहा, इसलिए अपने मनोगत भावों से न तो मैं ही स्वयं पूरी तरह परिचित हो पाया और न गांधारी ही हो पाई। यह अपरिचय मुझे भारी पड़ा। सबकुछ खोकर अब मन के अवगुंठन खोल रहा हूँ।
मेरे ऊपर दो कलंक लगाए जाते हैं—लाक्षागृह-कांड और द्यूत-सभा मं द्रौपदी का वस्त्र-हरण। पांडवों को वारणावत भेजने का प्रस्ताव दुर्योधन ने उनकी हस्तिनापुर में लोकप्रियता कम करने के उद्देश्य से रखा। लाक्षागृह में पांडवों को जीवित जलाने की योजना मुझसे और कर्ण से गोपनीय रखी गई।
दूसरे, आर्यों के अनेक व्यसनों में द्यूत-क्रीड़ा भी एक व्यसन था। युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया, वह आया, और खेला और सबकुछ हार गया। उसने स्वंय स्वीकार किया
कि जुएं में उससे छल-कपट नहीं किया गया। तत्समय मुद्र का अधिक प्रचलन नहीं था। ‘धन’ के अंतर्गत अर्थ, भूमि, गौ, स्वर्ण, विविध वस्तुएँ, पत्नी और आत्मीय जन आते थे। एक-एक कर सबको दाँव पर लगाना परंपरानुकूल था। द्रौपदी का वस्त्र-हरण और कृष्ण का वस्त्र-दान परवर्ती कल्पनाएँ हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर का संदेश पाकर स्वंय राजसभा में आयी थीं। वह राज-वस्त्र पहने थीं, पांडवों की तरह वे वस्त्र उतारकर दास-वस्त्र पहनने के लिए उनसे कहा गया। इसकी भरपाई में मैंने उसे वरदान दिए। उसे वरदान देते समय जो प्रकाश-किरण मेरे भीतर उतरी थी, वह बाद में लुप्त हो गई और मैं एक आदर्श वृद्ध से पुनः धृतराष्ट्र बन गया।
प्रत्येक सभ्य समाज में समन्वय, समरसता और लोक-संग्रह की संसिद्घि के लिए साधनों की पवित्रता पर बल दिया जाता है। ऐसा न होने पर विकृत स्थितियाँ उत्पन्न होती है जो नियंत्रक शक्तियों को हिला देती हैं। उस समय द्वापर में तो एक वंश नष्ट हो गया, लेकिन क्या वंशवाद समूल नष्ट होता है ? क्या राजनीतिक महत्वाकाक्षाएँ, बुद्धमूल स्वार्थी तंत्त्वों के नियोग से उसे सदा हरा-भरा नहीं रख सकतीं ? दुर्योधन का काल-निर्णय गलत था—उसने अयुद्ध की स्थिति में अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए भ्रष्ट साधन अपनाए परंतु युद्ध में उसने साधनों की पवित्रता पर ही जोर दिया।
अंत में, जीवन की सभी अवस्थाओं से गुजरकर राजा धृतराष्ट्र अपने ‘मैं’ से विलग होकर समरूप हो गया हूँ। भले ही कृष्म से अर्जुन कासाथ छूट गया परंतु संजय सदा मेरे साथ बना रहा—अंत तक। मैंने अपनी गाथा में स्व-छिद्रों को ढकने का प्रयास नहीं किया है। मुझे विश्वास है कि अपनी असफलताओं के मध्य से ही मैं सुधी पाठकों तक पहुँचूँगा आप न्यायाधीष हैं, मेरी गाथा आपके सामने है।
मेरे पुत्रों और पांडु-पुत्रों के मध्य वंश विभाजन की रेखा खींचना सरल नहीं है। पांडु-पुत्रों को पांडव तो कहा जा सकता है पर कौरव के वजन पर क्यों नहीं क्योंकि हमसे पंद्रहवीं पीढ़ी पूर्व हमारे वंश में कुरु नामक राजा हुए थे और उन्हीं के नाम पर कौरव वंश चला। अतः जैसे पांडु-पुत्रों का पितृवाचक नाम पांडव है वैसे ही मेरे पुत्रों का नाम ‘धार्तराष्ट्र’ हुआ। यह नाम अक्सर नहीं लिया जाता। इतिहास की जो वक्र रेखाएं हैं उन्हें सरल करना है मेरा ध्येय है।
मेरे जनक व्यासदेव ने मेरे साथ पूर्ण न्याय नहीं किया। कहा जाता है कि पिता के लिए दो पुत्र दोनों आँखों के समान होते हैं। पर कौन जानता है कि दोनों आँखों की दृश्य-शक्ति अक्सर बराबर नहीं होती उनकी भावनाओं का पलड़ा सदैव पांडु और उसके बाद उनके पुत्रों की ओर झुका रहा। जब संघर्ष की स्थिति आई तो वे उनके साथ खड़े दिखाई दिए। हमारा चित्र स्वयं धुंधला होता चला गया। यहाँ हमने विदुर की बात नहीं कही है। यथास्थान उनके प्रति हुए अन्याय की गाथा भी आपको सुनाऊँगा।
मैं और पांडु व्यास जी के क्षेत्रज पुत्र थे। उन्होंने न हमारा शैशव देखा, न कैशोर्य और न ही यौवन का प्रथम चरण। वे अपनी साधना में लीन रहे, अतः हमारी यह गाथा अपने ग्रंथ में समाहित नहीं कर सके। मेरा और पाडु का बचपन विस्मृति के गर्त में समाया है। मैं इसे बाहर लाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा।
कथा कहने की जो विधा आज प्रचलित है मेरा ढंग उससे भिन्न होगा। भई, मैं 3-4 हजार वर्ष पुराना जो हूँ। तत्समय पिता की या किसी अग्रज की उसी के मुख पर आलोचना करना अशिष्ट नहीं माना जाता था। दुर्योधन जब मेरी या विदुर की भर्त्सना करने लगे तो उसे कम से कम इस कारण अशिष्ट या धृष्ट नहीं समझना चाहिए मैं भी अपने जनक, जननी या पत्नी के प्रति असहिष्णु हो उठूँ तो मुझे क्षमा करते रहिएगा क्योंकि मेरी गाथा जड़ उपाख्यान नहीं है
प्रत्युत मानव जीवन में चिरकाल से प्रवाहमान धारा है। आप आधुनिक हैं अतः हमारी अनेक बातें आपको अविश्वसनीय लग सकती हैं। परंतु उन बातों पर उस काल के सर्वाधिक ज्ञानी व्यक्ति भी विश्वास करते थे क्योंकि वे ज्ञान से विज्ञान और ऊपर उठकर प्रज्ञान—स्वंय सहित संपूर्ण जीवन का अपने अंदर चेतन ज्ञान-तक पहुँच गए थे। आपका विज्ञान पूर्णता की यात्रा में है। जिस दिन चौथा आयाम ज्ञात हो जाएगा उस दिन आधुनिक जगत् समझ पाएगा कि व्यास की ‘दिव्य-दृष्टि’ क्या थी और उसे अस्थायी रूप से संजय को कैसे दिया गया; समस्त जगत् को अच्छी प्रकार से ज्यों का त्यों देखने की व्यास को प्राप्त ‘प्रतिस्मृति विद्या’ थी !
मेरी गाथा में अविश्वसनीयता के छिद्र दृष्टिगत हो सकते हैं। यह गाथा द्वापर युग की है। द्वार का अर्थ है ‘संदेह’ है। सच कहूँ तो उस समय का मानव संदेहशील हो उठा था, उसमें अविश्वास जड़ें जमाने लगा था, शारीरिक सुख की वासना प्रधान हो गई थी, भोग ही लक्ष्य बन गया था, भोग के लिए संचय प्रारंभ हो गया था, कष्ट-सहिष्मुता और त्याग का लोप हो चुका था। यह सब विकृतियाँ पल्लवित होकर आज भी तहलका मचा रही हैं, अंतर यही है कि उस समय व्यक्ति धर्मभीरु था, उसका उपार्जन पवित्र था। इसे पढ़कर ही आप समझ पाएँगे कि मैं खलरूप नहीं हूँ प्रत्युत ऐसा व्यक्ति हूँ जो अस्तित्व के अंधकार में भटकता हुआ प्रकाश के लिए पुत्ररूपी अग्निशिखा से लिपट जाता है। पुत्र-मोह मेरी जड़ता थी, देखता हूँ वैसी जड़ें आज भी उन्मीलित नहीं हो पाई हैं।
भाग्यवादी होने के कारण मैं किसी की महानता के शिखर पर नहीं पहुँच पाया। पांडु के उच्छिष्ट राज्य पर मैं रक्षक-सर्प बनकर जरूर बैठा परंतु उस पर अपने नैसर्गिक अधिकार का विष वमन करता रहा। महानता सत्ता में नहीं होती वह होती है संघर्ष में, लोक से संबंध होने में, पुरुषार्थ में, कर्म में, मुझे सत्ता मिली, मैं कर्म-च्युत हो गया—कुछ अपनी सोच के कारण शेष अपनी परिस्थितियों के वशीभूत होकर। मेरा सोच सदा यही रहा, ‘‘ब्रह्मा ने जो रच दिया है, सारा जगत् वैसी ही चेष्टा में लगा हुआ है।’
मैंने कई अवसरों पर इतिहास की अनिवार्यता को नकारा। राजा होने के नाते यदि मैं उन क्षणों को पकड़ पाता, मेरी प्रज्ञा स्थायी रहती तो मेरा काल-खंड इतिहास में श्लाघ्य होता। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मानव इतिहास में युद्ध से सर्वथा मुक्त एक भी युग नहीं दिखाई पड़ता और ऐसी पीढ़ियाँ शायद ही हों जिन्होंने संघर्ष के दर्शन न किए हों। समुद्र के नियमित ज्वार के समान ही संघर्षों की, युद्धों-महायुद्धों की तरंगे भी उठती-बैठती हैं।
परंतु मेरे जीवन में ज्वार तो आया पर उसका अवसान भाटा नहीं हुआ ! इतिहास ने सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया यदि मैंने दृढ़ इच्छा-शक्ति से काम लिया होता तो कृष्ण द्वारा प्रस्तुत संधि का अनुमोदन किया जा सकता था, युद्ध टल सकता था, कौरवों-पांडवों में सौमनस्य स्थापित हो सकता था, पांडवों को उनका राज्य वापस दिया जा सकता था। हाँ, यह सब मैं कर सकता था परंतु विवश था क्योंकि मैं वास्तविक शक्ति-केन्द्र नहीं रह गया था। मैं पांडवों को दोष नहीं देता, पर कहना पड़ेगा कि युद्ध की प्रथम भेरी उन्होंने ही बजाई। उन्होंने पहला शांतिदूत ब्राह्मण के रूप में भेजा। कृष्ण के मना करने पर भी पांडवों ने सैन्य संग्रह प्रारंभ कर दिया।
मैं नहीं जानता कि मेरा जीवन क्यों अशांत रहा, दुविधाग्रस्त रहा, शंकापूरित रहा, स्वार्थ से आवृत्त रहा, दीन बनकर जलता-कुढ़ता रहा ! पता नहीं क्यों मैं अंतर्मुखी होकर घुटन और आत्मपीड़न की अंध-गुफा में उतर जाता रहा ! पथभ्रष्ट महत्वाकांक्षाओं की चाह से संशप्त पुत्र के, या कहूँ दुर्योधन के मोह ने मुझे भीरु बना दिया, प्रज्ञांध बना दिया। पुत्र-मोह ने मेरे जीवन में अतलांत खाइयाँ पैदा कर दीं तो मैं निरपेक्षता की सम-भूमि पर कैसे चल पाता ? विदुर के नीति परक वचन भी मेरा भावांतरण नहीं कर पाए। न्याय के मार्ग पर मैं तभी चला जब मेरे शरीर में काँटे चुभे।
गांधारी की प्रेरणा से अनुप्राणित होकर मैंने कई बार धृतात्मा बनने का प्रयास किया, लोक-कल्याण की भद्र भावना ने अनुप्राणित होने की कामना की परंतु इस प्रयास या कामना के साथ फलवती चेष्टा का संयोग कभी नहीं हो पाया। खुलकर बात करने में सदा संकोच करता रहा, इसलिए अपने मनोगत भावों से न तो मैं ही स्वयं पूरी तरह परिचित हो पाया और न गांधारी ही हो पाई। यह अपरिचय मुझे भारी पड़ा। सबकुछ खोकर अब मन के अवगुंठन खोल रहा हूँ।
मेरे ऊपर दो कलंक लगाए जाते हैं—लाक्षागृह-कांड और द्यूत-सभा मं द्रौपदी का वस्त्र-हरण। पांडवों को वारणावत भेजने का प्रस्ताव दुर्योधन ने उनकी हस्तिनापुर में लोकप्रियता कम करने के उद्देश्य से रखा। लाक्षागृह में पांडवों को जीवित जलाने की योजना मुझसे और कर्ण से गोपनीय रखी गई।
दूसरे, आर्यों के अनेक व्यसनों में द्यूत-क्रीड़ा भी एक व्यसन था। युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया, वह आया, और खेला और सबकुछ हार गया। उसने स्वंय स्वीकार किया
कि जुएं में उससे छल-कपट नहीं किया गया। तत्समय मुद्र का अधिक प्रचलन नहीं था। ‘धन’ के अंतर्गत अर्थ, भूमि, गौ, स्वर्ण, विविध वस्तुएँ, पत्नी और आत्मीय जन आते थे। एक-एक कर सबको दाँव पर लगाना परंपरानुकूल था। द्रौपदी का वस्त्र-हरण और कृष्ण का वस्त्र-दान परवर्ती कल्पनाएँ हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर का संदेश पाकर स्वंय राजसभा में आयी थीं। वह राज-वस्त्र पहने थीं, पांडवों की तरह वे वस्त्र उतारकर दास-वस्त्र पहनने के लिए उनसे कहा गया। इसकी भरपाई में मैंने उसे वरदान दिए। उसे वरदान देते समय जो प्रकाश-किरण मेरे भीतर उतरी थी, वह बाद में लुप्त हो गई और मैं एक आदर्श वृद्ध से पुनः धृतराष्ट्र बन गया।
प्रत्येक सभ्य समाज में समन्वय, समरसता और लोक-संग्रह की संसिद्घि के लिए साधनों की पवित्रता पर बल दिया जाता है। ऐसा न होने पर विकृत स्थितियाँ उत्पन्न होती है जो नियंत्रक शक्तियों को हिला देती हैं। उस समय द्वापर में तो एक वंश नष्ट हो गया, लेकिन क्या वंशवाद समूल नष्ट होता है ? क्या राजनीतिक महत्वाकाक्षाएँ, बुद्धमूल स्वार्थी तंत्त्वों के नियोग से उसे सदा हरा-भरा नहीं रख सकतीं ? दुर्योधन का काल-निर्णय गलत था—उसने अयुद्ध की स्थिति में अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए भ्रष्ट साधन अपनाए परंतु युद्ध में उसने साधनों की पवित्रता पर ही जोर दिया।
अंत में, जीवन की सभी अवस्थाओं से गुजरकर राजा धृतराष्ट्र अपने ‘मैं’ से विलग होकर समरूप हो गया हूँ। भले ही कृष्म से अर्जुन कासाथ छूट गया परंतु संजय सदा मेरे साथ बना रहा—अंत तक। मैंने अपनी गाथा में स्व-छिद्रों को ढकने का प्रयास नहीं किया है। मुझे विश्वास है कि अपनी असफलताओं के मध्य से ही मैं सुधी पाठकों तक पहुँचूँगा आप न्यायाधीष हैं, मेरी गाथा आपके सामने है।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i