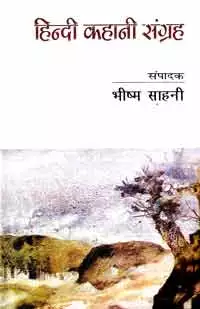|
कहानी संग्रह >> 10 प्रतिनिधि कहानियाँ (भीष्म साहनी) 10 प्रतिनिधि कहानियाँ (भीष्म साहनी)भीष्म साहनी
|
195 पाठक हैं |
|||||||
भीष्म साहनी के द्वारा चुनी हुई श्रेष्ठ दस कहानियाँ...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘दस प्रतिनिधि कहानियाँ’ सीरीज़ ‘किताबघर’ घर की एक महत्त्वाकांक्षी कथा-योजना है, जिसमें हिन्दी कथा-जगत के सभी शीर्षस्थ कथाकारों को प्रस्तुत किया जा रहा है।
इस सीरीज़ में सम्मिलित कहानीकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने सम्पूर्ण कथा-दौर से उन दस कहानियों का चयन करें जो पाठकों, समीक्षकों तथा संपादकों के लिए मील का पत्थर रही हों तथा ये ऐसी कहानियाँ भी हों जिनकी वजह से उन्हें स्वयं को भी कथाकार होने का अहसास बना रहा हो। भूमिका-स्वरूप लेखक का एक वक्तव्य भी इस सीरीज़ के लिए आमंत्रित किया गया जिसमें प्रस्तुत कहानियों को प्रतिनिधित्व सौंपने की बात पर चर्चा करना अपेक्षित रहा है।
‘किताबघर’ गौरवान्वित है कि इस सीरीज़ के लिए अग्रज कथाकारों का उसे सहज सहयोग मिला है। इस सीरीज़ के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कथाकार भीष्म साहनी ने प्रस्तुत संकलन में अपनी जिन दस कहानियों को प्रस्तुत किया है, वे हैं ; ‘वाङ्चू’, ‘साग-मीट’, पाली, ‘समाधि भाई रामसिंह’, ‘फूलाँ’, ‘सँभल के बाबू’, ‘आवाजें’, ‘तेंदुआ’, ‘ढ़ोलक’ तथा ‘साये’।
हमें विश्वास है कि इस सीरीज़ के माध्यम से पाठक सुविख्यात कथाकार भीष्म साहनी की प्रतिनिधि कहानियों को एक ही जिल्द में पाकर सुखद संतोष का अनुभव करेंगे।
इस सीरीज़ में सम्मिलित कहानीकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने सम्पूर्ण कथा-दौर से उन दस कहानियों का चयन करें जो पाठकों, समीक्षकों तथा संपादकों के लिए मील का पत्थर रही हों तथा ये ऐसी कहानियाँ भी हों जिनकी वजह से उन्हें स्वयं को भी कथाकार होने का अहसास बना रहा हो। भूमिका-स्वरूप लेखक का एक वक्तव्य भी इस सीरीज़ के लिए आमंत्रित किया गया जिसमें प्रस्तुत कहानियों को प्रतिनिधित्व सौंपने की बात पर चर्चा करना अपेक्षित रहा है।
‘किताबघर’ गौरवान्वित है कि इस सीरीज़ के लिए अग्रज कथाकारों का उसे सहज सहयोग मिला है। इस सीरीज़ के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कथाकार भीष्म साहनी ने प्रस्तुत संकलन में अपनी जिन दस कहानियों को प्रस्तुत किया है, वे हैं ; ‘वाङ्चू’, ‘साग-मीट’, पाली, ‘समाधि भाई रामसिंह’, ‘फूलाँ’, ‘सँभल के बाबू’, ‘आवाजें’, ‘तेंदुआ’, ‘ढ़ोलक’ तथा ‘साये’।
हमें विश्वास है कि इस सीरीज़ के माध्यम से पाठक सुविख्यात कथाकार भीष्म साहनी की प्रतिनिधि कहानियों को एक ही जिल्द में पाकर सुखद संतोष का अनुभव करेंगे।
मेरी कथा-यात्रा के निष्कर्ष
अपनी लम्बी-कथा यात्रा का लेखा-जोखा करना आसान काम नहीं है। पर यदि इस
सर्वेक्षण में से कुछेक प्रश्न निकाल दें—कि मैं लिखने की ओर
क्यों उन्मुख हुआ, और गद्य को ही अभिव्यक्ति का माध्यम क्यों चुना, और
उसमें भी कथा-कहानी ही को क्यों चुना—क्योंकि इस प्रकार के
प्रश्नों का उत्तर दे पाना स्वयं लेखक के लिए कठिन होता है—तो
सर्वेक्षण करना कुछ आसान भी हो जाता है। यदि कहानियों को केंद्र में ही
रखें, साथ ही अपने परिवेश को, और उन संस्कारों को जिनसे लेखक के प्रारंभिक
वर्ष प्रभावित हुए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी साथ-साथ मिलने लगते
हैं।
मेरी अधिकांश कहानियां यथार्थपरक रही हैं, मात्र व्यक्ति केन्द्रित अथवा व्यक्ति के अन्तर्मन पर केंद्रित ही नहीं रही हैं, कहीं-न-कहीं मेरे पात्रों के व्यवहार तथा गतिविधि पर बाहर की गतिविधि का गहरा प्रभाव रहा है। बल्कि यदि यह कहें कि जिस विसंगति अथवा अंतर्विरोध को लेकर कहानी लिखी गई, वह मात्र व्यक्ति की स्थिति का अंतर्विरोध न होकर, उसके आसपास के सामाजिक जीवन का अंतर्विरोध होकर उसके व्यक्तिगत जीवन में लक्षित होता है तो कहना अधिक उपयुक्त होगा।
यों तो जब हम किसी व्यक्ति की कहानी कहते हैं तो वह मात्र एक की कहानी नहीं होती, उसमें एक प्रकार की व्यापकता आ जाती है। उसकी मानसिकता, उसकी दृष्टि, उसका संघर्ष आदि मात्र उसका न रहकर आज के आदमी का बन जाता है। वह पात्र अपने काल का प्रतिनिधि बन जाता है। इसी कारण लोग इन कहानियों को पढ़ते भी हैं क्योंकि इनमें उन्हें अपने काल के सामान्य जीवन का बिम्ब देखने को मिलता है।
अब अपने परिवेश में से लेखक क्या चुनता है और क्या छोड़ देता है, किस पहलू की ओर वह अधिक आकृष्ट होता है, कौन-सा पहलू उसे अधिक उद्वेलित करता है, किसके साथ वह भावनात्मक स्तर पर जुड़ता है, तो वह निश्चय ही हम उसके लेखकीय व्यक्तित्व को अधिक स्पष्टता से जान-समझ पाते हैं। स्त्री-पुरुष के यौन-संबंध भी एक पहलू हैं, गरीबी भी एक पहलू है, मनुष्य के मस्तिष्क को उकसानेवाले विचार और विचारधाराएँ भी एक पहलू हैं, ऐसे पहलुओं का कोई अन्त नहीं, और जब इनका आग्रह लेखक की जिंदगी को देखने और उसमें से लेखन-कर्म के लिए कच्चा माल चुनने-उठाने में मदद करता है, तो धीरे-धीरे लेखक का लेखकीय व्यक्तित्व रूप लेने लगता है।
बचपन के संस्कार, जिस वायुमंडल में आपका शैशवकाल बीता है, लेखक के दृष्टि-निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
दूर बचपन में, रात को खाना खा चुकने पर परिवार के लोग बड़े कमरे में आ जाते। दोनों बहनें बगलवाले कमरे में चली जातीं, क्योंकि दूसरे दिन सुबह उन्हें स्कूल जाना होता था, हम दोनों भाई उसी बड़े कमरे में एक पलंग पर लेट जाते। पिताजी कमरे में ऊपर-नीचे टहलते और तरह-तरह की घटनाओं पर टिप्पणी करते। अक्सर इन बातों का संबंध बाहर की दुनिया से होता और पिताजी बोलते-बोलते अक्सर उत्तेजित हो उठते थे, उनकी बातें तो पूरी तरह से समझ में नहीं आती थीं पर उनकी उत्तेजना जरूर मन पर असर करती। कभी कहते : अंग्रेजों ने देश को लूट खाया है। कभी समाज-सुधार की बातें करते। मैं इन बातों को समझ तो नहीं पाता था, पर मेरे भीतर कहीं उनकी उत्कट भावना अपना प्रभाव छोड़ जाती थी, अक्सर ऐसा होता था। बचपन में हमारा मस्तिष्क समझ भले ही न पाता हो, पर हमारा संवेदन निश्चय ही उद्वेलित होता है। फिर बहुत कुछ है जो हम देखते हैं। मैं छोटा-सा था जब मुहल्लेवालों ने एक आदमी को पकड़ लिया और उसे बिजली के खम्भे के साथ बाँधने लगे। उसे इस जोर से बाँधा कि उसकी आँखें निकल आईं। इस पर थप्पड़ और घूँसे अलग। उसे अधमरा करके छोड़ा। गली में अक्सर शोर होता था। फैज़अली नाम का एक आदमी एक रात कुल्हाड़ी लेकर एक घर के बाहर जा पहुँचा, जहाँ उसी के रिश्ते के दो वयोवृद्ध पति-पत्नी रहते थे। यों भी रात के सन्नाटे में किसी का चिल्लाना सुनकर दिल दहल जाता है, फैज़अली दरवाज़े पर कुल्हाड़ी से बार-बार वार करता, साथ में ऊँची आवाज़ में गालियाँ बकता। घर के निकट ही एक बड़ा मैदान था जहाँ जाड़े के दिनों में हर इतवार को कुत्तों की लड़ाई का आयोजन किया जाता। लोग शर्तें बाँधते। पले हुए शिकारी कुत्ते एक-दूसरे पर छोड़ दिये जाते। वे एक-दूसरे को नोचते, फिर एक जख्मी कुत्ता मुकाबला न कर पाने पर वहाँ से भागना चाहता पर जिन लोगों ने शर्तें बाँध रखी होतीं, वे उसे भागने नहीं देते थे और उस पर पत्थर फेंक-फेंककर उसे वापस प्रतिस्पर्धी के सामने भेजते। और कई बार आपस में लड़ने लगते।
मैं ग्यारह वर्ष का था जब हमारे शहर में पहला हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ था। तब मैंने पहली बार ऊँची उठती आग की लपटें देखी थीं जिनसे आधा आसमान लाल हो गया था।
ऐसे अनुभव निश्चय ही अपना प्रभाव छोड़ जाते। बचपन में हर दिन नये-नये अनुभव लाता है, आप पहली बार अपने परिवेश पर आँखें खोल रहे होते हैं। एक संसार घर के बाहर का, एक घर के अंदर का। घर के अंदर रिश्तों-संबंधों का प्रभाव, भाई-भाई का, माँ-बाप का आदि-आदि। तरह-तरह का हृदयग्राही अनुभवों की गोद में हमारा बचपन बीतता है और जीवन के पहले अनुभव होने के नाते वे अविस्मरणीय होते हैं।
मैंने कुछ विस्तार से इनकी चर्चा की पर अनुभवों का संग्रह तो आजीवन बढ़ता जाता है। केवल बचपन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं, दृष्टि भी किसी हद तक देते हैं।
समय आने पर कभी हम उन परिस्थितियों के प्रति विद्रोह करने लगते हैं और कभी उनके अनुसार अपने को ढाल लेते हैं।
किसी लेखक का संवेदन किस भाँति व्यक्तित्व ग्रहण करता है, यह बड़ा पेचीदा सवाल है। मैंने केवल इसके एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश की है कि मेरा लेखन समाजोन्मुख क्योंकर हुआ। यों तो अपनी वकालत करते हुए मैं यह भी कहता हूँ कि जिस कालखंड में हम जी रहे हैं, उसमें लेखक बाह्योन्मुख होने पर मजबूर भी हो जाता है। हिरोशिमा पर आणविक बम गिराया गया तो दुनियाभर के लोगों के दिल दहल गए। आये दिन जो रेडियो-टेलीविज़न पर देश-विदेश की खबरें सुनते हैं वे हमारे संवेदन को खरोंचे बिना नहीं रह सकतीं। और मेरा तो यह भी मानना है कि हमारे यहाँ भारत में साहित्य, उन्नीसवीं शताब्दी से ही यथार्थोन्मुख और समाजोन्मुख होने लगा था। इसकी एक कड़ी बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय, फिर भारतेन्दु और फिर प्रेमचन्द आदि थे।
पर यह सब मेरी अपनी वकालत की बात है, प्रत्येक लेखक अन्ततः अपने संवेदन, अपनी दृष्टि, जीवन की अपनी समझ के अनुसार लिखता है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि मात्र विचारों के बल पर लिखी गई रचना जिसके पीछे जीवन का प्रामाणिक अनुभव न हो, अक्सर अधकचरी रह जाती है।
अपनी सफाई में एक और बात कह दूँ। मेरी धारणा है कि साहित्य के केन्द्र में मानव है, व्यक्ति है, परन्तु वह व्यक्ति अलग-थलग नहीं है—अपने में सम्पूर्ण इकाई नहीं है। उसे समझ पाने के लिए उसे उसके परिवेश में रखना भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बहुत हद तक वह अपने परिवेश के साथ की उपज भी होता है। पर वह अपने परिवेश के हाथ की कठपुतली नहीं होता। वह अपने परिवेश से जहाँ बहुत कुछ लेता है, वहाँ वह बहुत कुछ को रद्द भी कर देता है। यदि लेखक की साहित्य-यात्रा को सत्य की खोज का नाम दें तो वह गलत नहीं होगा। लेखक की कलम का लिखा प्रत्येक वाक्य एक तरह से सत्य की खोज में अग्रसर हो रहा होता है। जीवन-दर्शन भी कराता है तो उसके पीछे यह आग्रह रहता है कि जीवन की सच्चाई तक पहुँच पाये और उसे उघाड़कर पाठक के सामने रख दे। इसे भी मैं लेखक के संवेदन का नैसर्गिक गुण मानता हूँ। जीवन का कोई अंतर्विरोध जब उसे कलम उठाने पर बाध्य करता है तो उसी क्षण वह उस अंतर्विरोध की तह तक पहुँचने की कोशिश करने लगता है और उसमें लाग-लपेट की बात नहीं रहती। वह न तो अपने को झुठला सकता है, न ही पाठक को, जहाँ झुठलाने लगता है, वहाँ रचना भी झूठी पड़ने लगती है।
इस प्रश्न का—कि लेखक क्यों लिखता है—उत्तर भी शायद इससे मिल जाए। जब कोई छोटा-सा बच्चा कागज-पेंसिल लेकर कागज पर बिल्ली का चित्र रेखांकित बनाता है, तो उसके पीछे जीवन की अनुकृति पेश कर पाने का आग्रह सर्वोपरि रहता है। शायद लेखक के प्रभाव के पीछे भी ऐसा ही आग्रह काम कर रहा होता है। जीवन के किसी पहलू ने जैसी छाप उसके मन में छोड़ी है, उसकी अनुकृति पेश कर पाने का आग्रह। वैसा ही आग्रह अभिनय में भी रहता है। छोटा बच्चा नकल उतारता है, कभी वेशभूषा बदलकर साधु बन जाता है, कभी पुलिसमैन, तो वहाँ भी आग्रह जीवन की अनुकृति पेश करता ही रहता है।
साहित्य में और जीवन में एक बहुत बड़ा अन्तर भी है। साहित्य में सम्भावनाएँ प्रमुख होती हैं, यदि साहित्य हमारा जीवन के यथार्थ से साक्षात् भी कराता है तो मुख्यतः भावनाओं के माध्यम से। पर जीवन का व्यवहार मात्र भावनाओं के आधार पर नहीं चलता। वहाँ अपना हित, स्वार्थ, व्यवहारकुशलता, निर्मम होड़ की भावना आदि सब काम आते हैं। यही कारण है कि रोमांटिक हीरो उपन्यास में तो प्रभावित करता है, यथार्थ जीवन में भी यदि वह वैसा ही व्यवहार करने लगे तो बड़ा असंगत और अटपटा लगने लगता है। भावावेश में किया गया व्यवहार उपन्यास में जँचता है, परन्तु यथार्थ के ठोस धरातल पर नहीं जँचता। यहाँ तक कि आदर्शवादिता कहानी-उपन्यास में तो जीवन का एक मूल्य बनकर आती है, पर यथार्थ जीवन में आदर्शवादी व्यक्ति अक्सर पिछड़ा व्यक्ति ही माना जाता है। यथार्थ जीवन में अपनी जगह बना पाने के लिए जागरुकता, स्वार्थपरता, अपने को आगे बढ़ाने की उत्कट इच्छा आदि की ज़रूरत रहती है। इसीलिए जीवन के यथार्थ और साहित्य के यथार्थ में एक अंतर होता है। वास्तविकता की झलक तो साहित्य में ज़रूर मिलती है, पर साहित्य मूल्यों से जुड़ा होता है। इसलिए आदर्शवादिता के लिए साहित्य में तो बहुत बड़ा स्थान होता है, पर व्यावहारिक जीवन में नहीं। इन मूल्यों में मानवीयता सबसे बड़ा मूल्य है। इस दृष्टि से साहित्य यथार्थ से जुड़ता हुआ भी यथार्थ से ऊपर उठ जाता है, लेखक यथार्थ का चित्रण करते हुए भी पाठक को यथार्थेतर स्तर तक ले जाता है जहाँ हम यथार्थ जीवन की गतिविधि को मूल्यों की कसौटी पर आँकते हैं। जीवन को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इनमें सच्चाई के अतिरिक्त न्यायपरता और जनहित, और मानवीयता आदि भी आ जाते हैं। मात्र यथार्थ की कसौटी पर ही सही साबित होने वाली रचना हमें आश्वस्त नहीं करती। उसमें मानवीयता तथा उससे जुड़े अन्य मूल्यों का समावेश आवश्यक होता है। और रचना जितना ऊँचा हमें ले जाए, जितनी विशाल व्यापक दृष्टि हमें दे पाए उतनी ही वह रचना हमारे लिए मूल्यवान होगी।
यह तो रही साहित्य-विवेचन की बात।
अन्त में, लेखक के साहित्यिक प्रयास कहाँ तक सफल हो पाए हैं, कहाँ तक उन्हें सत्प्रयास कहा जा सकता है, कहाँ तक वे साहित्य की माँगों को पूरा कर पाए हैं, इसका फैसला तो पाठकगण ही करेंगे।
धीरे-धीरे अपने विशेष आग्रहों के अनुरूप लिखते हुए, लेखक का छोटा-मोटा व्यक्तित्व—सृजनात्मक व्यक्तित्व—बनने लगता है। उसकी रचनाओं में कुछेक विशिष्टताओं की झलक मिलने लगती है। यही विशिष्टताएँ उसकी पहचान बन जाती हैं। परन्तु धीरे-धीरे वही विशिष्टता उसकी सीमा भी बनने लगती है। एक ही तरह की कहानियाँ लिखते हुए वह अपने को दोहराने भी लगता है, उसकी रचनाओं से एक ही प्रकार की ध्वनि सुनाई देने लगती है। पहले जो उसकी विशिष्टता थी वही अब उसका ढर्रा बन चुकी होती है। लेखक के लिए यह स्थिति बड़ी शोचनीय होती है। नई जमीन को तोड़ना, ज़िंदगी नये-नये मोड़ काटती रहती है, उसके प्रति जागरुक रहना, विचारों के धरातल पर जड़ता को न आने देना, यह भी लेखक के लिए उतना ही बड़ा दायित्व होता है, यह भी सत्य के अन्वेषण और सत्य की खोज का अंग है। वह अपने संवेदन को जंग नहीं लगने दे, इसके लिए उन्मुक्त, संतुलित स्वच्छन्द दृष्टि को बनाए रखे, संवेदन के स्तर पर ग्रहणशील बना रहे, यह नितांत आवश्यक है।
ऐसे ही कुछ निष्कर्ष हैं जो अपनी कथा-यात्रा में मैंने ग्रहण किए हैं।
अस्तु !
मेरी अधिकांश कहानियां यथार्थपरक रही हैं, मात्र व्यक्ति केन्द्रित अथवा व्यक्ति के अन्तर्मन पर केंद्रित ही नहीं रही हैं, कहीं-न-कहीं मेरे पात्रों के व्यवहार तथा गतिविधि पर बाहर की गतिविधि का गहरा प्रभाव रहा है। बल्कि यदि यह कहें कि जिस विसंगति अथवा अंतर्विरोध को लेकर कहानी लिखी गई, वह मात्र व्यक्ति की स्थिति का अंतर्विरोध न होकर, उसके आसपास के सामाजिक जीवन का अंतर्विरोध होकर उसके व्यक्तिगत जीवन में लक्षित होता है तो कहना अधिक उपयुक्त होगा।
यों तो जब हम किसी व्यक्ति की कहानी कहते हैं तो वह मात्र एक की कहानी नहीं होती, उसमें एक प्रकार की व्यापकता आ जाती है। उसकी मानसिकता, उसकी दृष्टि, उसका संघर्ष आदि मात्र उसका न रहकर आज के आदमी का बन जाता है। वह पात्र अपने काल का प्रतिनिधि बन जाता है। इसी कारण लोग इन कहानियों को पढ़ते भी हैं क्योंकि इनमें उन्हें अपने काल के सामान्य जीवन का बिम्ब देखने को मिलता है।
अब अपने परिवेश में से लेखक क्या चुनता है और क्या छोड़ देता है, किस पहलू की ओर वह अधिक आकृष्ट होता है, कौन-सा पहलू उसे अधिक उद्वेलित करता है, किसके साथ वह भावनात्मक स्तर पर जुड़ता है, तो वह निश्चय ही हम उसके लेखकीय व्यक्तित्व को अधिक स्पष्टता से जान-समझ पाते हैं। स्त्री-पुरुष के यौन-संबंध भी एक पहलू हैं, गरीबी भी एक पहलू है, मनुष्य के मस्तिष्क को उकसानेवाले विचार और विचारधाराएँ भी एक पहलू हैं, ऐसे पहलुओं का कोई अन्त नहीं, और जब इनका आग्रह लेखक की जिंदगी को देखने और उसमें से लेखन-कर्म के लिए कच्चा माल चुनने-उठाने में मदद करता है, तो धीरे-धीरे लेखक का लेखकीय व्यक्तित्व रूप लेने लगता है।
बचपन के संस्कार, जिस वायुमंडल में आपका शैशवकाल बीता है, लेखक के दृष्टि-निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
दूर बचपन में, रात को खाना खा चुकने पर परिवार के लोग बड़े कमरे में आ जाते। दोनों बहनें बगलवाले कमरे में चली जातीं, क्योंकि दूसरे दिन सुबह उन्हें स्कूल जाना होता था, हम दोनों भाई उसी बड़े कमरे में एक पलंग पर लेट जाते। पिताजी कमरे में ऊपर-नीचे टहलते और तरह-तरह की घटनाओं पर टिप्पणी करते। अक्सर इन बातों का संबंध बाहर की दुनिया से होता और पिताजी बोलते-बोलते अक्सर उत्तेजित हो उठते थे, उनकी बातें तो पूरी तरह से समझ में नहीं आती थीं पर उनकी उत्तेजना जरूर मन पर असर करती। कभी कहते : अंग्रेजों ने देश को लूट खाया है। कभी समाज-सुधार की बातें करते। मैं इन बातों को समझ तो नहीं पाता था, पर मेरे भीतर कहीं उनकी उत्कट भावना अपना प्रभाव छोड़ जाती थी, अक्सर ऐसा होता था। बचपन में हमारा मस्तिष्क समझ भले ही न पाता हो, पर हमारा संवेदन निश्चय ही उद्वेलित होता है। फिर बहुत कुछ है जो हम देखते हैं। मैं छोटा-सा था जब मुहल्लेवालों ने एक आदमी को पकड़ लिया और उसे बिजली के खम्भे के साथ बाँधने लगे। उसे इस जोर से बाँधा कि उसकी आँखें निकल आईं। इस पर थप्पड़ और घूँसे अलग। उसे अधमरा करके छोड़ा। गली में अक्सर शोर होता था। फैज़अली नाम का एक आदमी एक रात कुल्हाड़ी लेकर एक घर के बाहर जा पहुँचा, जहाँ उसी के रिश्ते के दो वयोवृद्ध पति-पत्नी रहते थे। यों भी रात के सन्नाटे में किसी का चिल्लाना सुनकर दिल दहल जाता है, फैज़अली दरवाज़े पर कुल्हाड़ी से बार-बार वार करता, साथ में ऊँची आवाज़ में गालियाँ बकता। घर के निकट ही एक बड़ा मैदान था जहाँ जाड़े के दिनों में हर इतवार को कुत्तों की लड़ाई का आयोजन किया जाता। लोग शर्तें बाँधते। पले हुए शिकारी कुत्ते एक-दूसरे पर छोड़ दिये जाते। वे एक-दूसरे को नोचते, फिर एक जख्मी कुत्ता मुकाबला न कर पाने पर वहाँ से भागना चाहता पर जिन लोगों ने शर्तें बाँध रखी होतीं, वे उसे भागने नहीं देते थे और उस पर पत्थर फेंक-फेंककर उसे वापस प्रतिस्पर्धी के सामने भेजते। और कई बार आपस में लड़ने लगते।
मैं ग्यारह वर्ष का था जब हमारे शहर में पहला हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ था। तब मैंने पहली बार ऊँची उठती आग की लपटें देखी थीं जिनसे आधा आसमान लाल हो गया था।
ऐसे अनुभव निश्चय ही अपना प्रभाव छोड़ जाते। बचपन में हर दिन नये-नये अनुभव लाता है, आप पहली बार अपने परिवेश पर आँखें खोल रहे होते हैं। एक संसार घर के बाहर का, एक घर के अंदर का। घर के अंदर रिश्तों-संबंधों का प्रभाव, भाई-भाई का, माँ-बाप का आदि-आदि। तरह-तरह का हृदयग्राही अनुभवों की गोद में हमारा बचपन बीतता है और जीवन के पहले अनुभव होने के नाते वे अविस्मरणीय होते हैं।
मैंने कुछ विस्तार से इनकी चर्चा की पर अनुभवों का संग्रह तो आजीवन बढ़ता जाता है। केवल बचपन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं, दृष्टि भी किसी हद तक देते हैं।
समय आने पर कभी हम उन परिस्थितियों के प्रति विद्रोह करने लगते हैं और कभी उनके अनुसार अपने को ढाल लेते हैं।
किसी लेखक का संवेदन किस भाँति व्यक्तित्व ग्रहण करता है, यह बड़ा पेचीदा सवाल है। मैंने केवल इसके एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश की है कि मेरा लेखन समाजोन्मुख क्योंकर हुआ। यों तो अपनी वकालत करते हुए मैं यह भी कहता हूँ कि जिस कालखंड में हम जी रहे हैं, उसमें लेखक बाह्योन्मुख होने पर मजबूर भी हो जाता है। हिरोशिमा पर आणविक बम गिराया गया तो दुनियाभर के लोगों के दिल दहल गए। आये दिन जो रेडियो-टेलीविज़न पर देश-विदेश की खबरें सुनते हैं वे हमारे संवेदन को खरोंचे बिना नहीं रह सकतीं। और मेरा तो यह भी मानना है कि हमारे यहाँ भारत में साहित्य, उन्नीसवीं शताब्दी से ही यथार्थोन्मुख और समाजोन्मुख होने लगा था। इसकी एक कड़ी बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय, फिर भारतेन्दु और फिर प्रेमचन्द आदि थे।
पर यह सब मेरी अपनी वकालत की बात है, प्रत्येक लेखक अन्ततः अपने संवेदन, अपनी दृष्टि, जीवन की अपनी समझ के अनुसार लिखता है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि मात्र विचारों के बल पर लिखी गई रचना जिसके पीछे जीवन का प्रामाणिक अनुभव न हो, अक्सर अधकचरी रह जाती है।
अपनी सफाई में एक और बात कह दूँ। मेरी धारणा है कि साहित्य के केन्द्र में मानव है, व्यक्ति है, परन्तु वह व्यक्ति अलग-थलग नहीं है—अपने में सम्पूर्ण इकाई नहीं है। उसे समझ पाने के लिए उसे उसके परिवेश में रखना भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बहुत हद तक वह अपने परिवेश के साथ की उपज भी होता है। पर वह अपने परिवेश के हाथ की कठपुतली नहीं होता। वह अपने परिवेश से जहाँ बहुत कुछ लेता है, वहाँ वह बहुत कुछ को रद्द भी कर देता है। यदि लेखक की साहित्य-यात्रा को सत्य की खोज का नाम दें तो वह गलत नहीं होगा। लेखक की कलम का लिखा प्रत्येक वाक्य एक तरह से सत्य की खोज में अग्रसर हो रहा होता है। जीवन-दर्शन भी कराता है तो उसके पीछे यह आग्रह रहता है कि जीवन की सच्चाई तक पहुँच पाये और उसे उघाड़कर पाठक के सामने रख दे। इसे भी मैं लेखक के संवेदन का नैसर्गिक गुण मानता हूँ। जीवन का कोई अंतर्विरोध जब उसे कलम उठाने पर बाध्य करता है तो उसी क्षण वह उस अंतर्विरोध की तह तक पहुँचने की कोशिश करने लगता है और उसमें लाग-लपेट की बात नहीं रहती। वह न तो अपने को झुठला सकता है, न ही पाठक को, जहाँ झुठलाने लगता है, वहाँ रचना भी झूठी पड़ने लगती है।
इस प्रश्न का—कि लेखक क्यों लिखता है—उत्तर भी शायद इससे मिल जाए। जब कोई छोटा-सा बच्चा कागज-पेंसिल लेकर कागज पर बिल्ली का चित्र रेखांकित बनाता है, तो उसके पीछे जीवन की अनुकृति पेश कर पाने का आग्रह सर्वोपरि रहता है। शायद लेखक के प्रभाव के पीछे भी ऐसा ही आग्रह काम कर रहा होता है। जीवन के किसी पहलू ने जैसी छाप उसके मन में छोड़ी है, उसकी अनुकृति पेश कर पाने का आग्रह। वैसा ही आग्रह अभिनय में भी रहता है। छोटा बच्चा नकल उतारता है, कभी वेशभूषा बदलकर साधु बन जाता है, कभी पुलिसमैन, तो वहाँ भी आग्रह जीवन की अनुकृति पेश करता ही रहता है।
साहित्य में और जीवन में एक बहुत बड़ा अन्तर भी है। साहित्य में सम्भावनाएँ प्रमुख होती हैं, यदि साहित्य हमारा जीवन के यथार्थ से साक्षात् भी कराता है तो मुख्यतः भावनाओं के माध्यम से। पर जीवन का व्यवहार मात्र भावनाओं के आधार पर नहीं चलता। वहाँ अपना हित, स्वार्थ, व्यवहारकुशलता, निर्मम होड़ की भावना आदि सब काम आते हैं। यही कारण है कि रोमांटिक हीरो उपन्यास में तो प्रभावित करता है, यथार्थ जीवन में भी यदि वह वैसा ही व्यवहार करने लगे तो बड़ा असंगत और अटपटा लगने लगता है। भावावेश में किया गया व्यवहार उपन्यास में जँचता है, परन्तु यथार्थ के ठोस धरातल पर नहीं जँचता। यहाँ तक कि आदर्शवादिता कहानी-उपन्यास में तो जीवन का एक मूल्य बनकर आती है, पर यथार्थ जीवन में आदर्शवादी व्यक्ति अक्सर पिछड़ा व्यक्ति ही माना जाता है। यथार्थ जीवन में अपनी जगह बना पाने के लिए जागरुकता, स्वार्थपरता, अपने को आगे बढ़ाने की उत्कट इच्छा आदि की ज़रूरत रहती है। इसीलिए जीवन के यथार्थ और साहित्य के यथार्थ में एक अंतर होता है। वास्तविकता की झलक तो साहित्य में ज़रूर मिलती है, पर साहित्य मूल्यों से जुड़ा होता है। इसलिए आदर्शवादिता के लिए साहित्य में तो बहुत बड़ा स्थान होता है, पर व्यावहारिक जीवन में नहीं। इन मूल्यों में मानवीयता सबसे बड़ा मूल्य है। इस दृष्टि से साहित्य यथार्थ से जुड़ता हुआ भी यथार्थ से ऊपर उठ जाता है, लेखक यथार्थ का चित्रण करते हुए भी पाठक को यथार्थेतर स्तर तक ले जाता है जहाँ हम यथार्थ जीवन की गतिविधि को मूल्यों की कसौटी पर आँकते हैं। जीवन को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इनमें सच्चाई के अतिरिक्त न्यायपरता और जनहित, और मानवीयता आदि भी आ जाते हैं। मात्र यथार्थ की कसौटी पर ही सही साबित होने वाली रचना हमें आश्वस्त नहीं करती। उसमें मानवीयता तथा उससे जुड़े अन्य मूल्यों का समावेश आवश्यक होता है। और रचना जितना ऊँचा हमें ले जाए, जितनी विशाल व्यापक दृष्टि हमें दे पाए उतनी ही वह रचना हमारे लिए मूल्यवान होगी।
यह तो रही साहित्य-विवेचन की बात।
अन्त में, लेखक के साहित्यिक प्रयास कहाँ तक सफल हो पाए हैं, कहाँ तक उन्हें सत्प्रयास कहा जा सकता है, कहाँ तक वे साहित्य की माँगों को पूरा कर पाए हैं, इसका फैसला तो पाठकगण ही करेंगे।
धीरे-धीरे अपने विशेष आग्रहों के अनुरूप लिखते हुए, लेखक का छोटा-मोटा व्यक्तित्व—सृजनात्मक व्यक्तित्व—बनने लगता है। उसकी रचनाओं में कुछेक विशिष्टताओं की झलक मिलने लगती है। यही विशिष्टताएँ उसकी पहचान बन जाती हैं। परन्तु धीरे-धीरे वही विशिष्टता उसकी सीमा भी बनने लगती है। एक ही तरह की कहानियाँ लिखते हुए वह अपने को दोहराने भी लगता है, उसकी रचनाओं से एक ही प्रकार की ध्वनि सुनाई देने लगती है। पहले जो उसकी विशिष्टता थी वही अब उसका ढर्रा बन चुकी होती है। लेखक के लिए यह स्थिति बड़ी शोचनीय होती है। नई जमीन को तोड़ना, ज़िंदगी नये-नये मोड़ काटती रहती है, उसके प्रति जागरुक रहना, विचारों के धरातल पर जड़ता को न आने देना, यह भी लेखक के लिए उतना ही बड़ा दायित्व होता है, यह भी सत्य के अन्वेषण और सत्य की खोज का अंग है। वह अपने संवेदन को जंग नहीं लगने दे, इसके लिए उन्मुक्त, संतुलित स्वच्छन्द दृष्टि को बनाए रखे, संवेदन के स्तर पर ग्रहणशील बना रहे, यह नितांत आवश्यक है।
ऐसे ही कुछ निष्कर्ष हैं जो अपनी कथा-यात्रा में मैंने ग्रहण किए हैं।
अस्तु !
भीष्म साहनी
वाङ्चू
तभी दूर से वाङ्चू आता दिखाई दिया।
नदी के किनारे, लालमण्डी की सड़क पर धीरे-धीरे डोलता-सा चला आ रहा था। धूसर रंग का चोगा पहने था और दूर से लगता था कि बौद्ध भिक्षुओं की ही भाँति उसका सिर भी घुटा हुआ है। पीछे शंकराचार्य की ऊँची पहाड़ी थी और ऊपर स्वच्छ नीला आकाश। सड़क के दोनों ओर ऊँचे-ऊँचे सफेदे के पेड़ों की कतारें। क्षण-भर के लिए मुझे लगा, जैसे वाङ्चू इतिहास के पन्नों पर से उतर कर आ गया है। प्राचीन काल में इसी भाँति देश-विदेश से आने वाले चीवरधारी भिक्षु पहाड़ों और घाटियों को लाँघकर भारत में आया करते होंगे। अतीत के ऐसे ही रोमांचकारी धुँधलके में मुझे वाङ्चू भी चलता हुआ नजर आया। जब से वह श्रीनगर में आया था, बौद्ध विहारों के खंडहरों और संग्रहालयों में घूम रहा था। इस समय भी वह लालमण्डी के संग्रहालय में से निकलकर आ रहा था, जहाँ बौद्धकाल के अनेक अवशेष रखे हैं। उसकी मनःस्थिति को देखते हुए वह सचमुच ही वर्तमान से कटकर अतीत के ही किसी कालखण्ड में विचर रहा था।
‘‘बोधिसत्त्वों से भेंट हो गई ?’’ पास आने पर मैंने चुटकी ली।
वह मुस्करा दिया, हल्की टेढ़ी-सी मुस्कान, जिसे मेरी मौसेरी बहन डेढ़ दाँत की मुस्कान कहा करती थी, क्योंकि मुस्कराते वक्त वाङ्चू का ऊपर का होंठ केवल एक ओर से थोड़ा-सा ऊपर उठता था।
‘‘संग्रहालय के बाहर बहुत-सी मूर्तियाँ रखी हैं। मैं वही देखता रहा।’’ उसने धीमे से कहा, फिर वह सहसा भावुक होकर बोला, ‘‘एक मूर्ति के केवल पैर ही पैर बचे हैं....’’
मैंने सोचा, आगे कुछ कहेगा, परन्तु वह इतना भावविह्वल हो उठा था कि उसका गला रुँध गया और उसके लिए बोलना असम्भव हो गया।
हम एक साथ घर की ओर लौटने लगे।
‘‘महाप्राण के भी पैर ही पहले दिखाए जाते हैं।’’ उसने काँपती-सी आवाज में कहा और अपना हाथ मेरी कोहनी पर रख दिया। उसके हाथ का हल्का-सा कम्पन धड़कते दिल की तरह महसूस हो रहा था।
‘‘आरम्भ में महाप्राण की मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती थीं ना ! तुम तो जानते हो, पहले स्तूप के नीचे केवल पैर ही दिखाए जाते थे। मूर्तियाँ तो बाद में बनाई जाने लगी थीं।’’
जाहिर है, बोधिसत्त्व के पैर देखकर उसे महाप्राण के पैर याद आए थे और वह भावुक हो उठा था। कुछ पता नहीं चलता था, कौन-सी बात किस वक्त वाङ्चू को पुलकाने लगे, किस वक्त वह गदगद होने लगे।
‘‘तुमने बहुत देर कर दी। सभी लोग तुम्हारा इन्तजार कर रहे हैं। मैं चिनारों के नीचे भी तुम्हें खोज आया हूँ।’’ मैंने कहा।
‘‘मैं संग्रहालय में था...’’
‘‘वह तो ठीक है, पर दो बजे तक हमें हब्बाकदल पहुँच जाना चाहिए, वरना जाने का कोई लाभ नहीं।’’
उसने छोटे-छोटे झटकों के साथ तीन बार सिर हिलाया और कदम बढ़ा दिए।
वाङ्चू भारत में मतवाला घूम रहा था। वह महाप्राण के जन्म स्थान लुम्बिनी की यात्रा नंगे पाँव कर चुका था, सारा रास्ता हाथ जोड़े हुए। जिस-जिस दिशा में महाप्राण के चरण उठे थे, वाङ्चू मन्त्रमुग्ध-सा उसी-उसी दिशा में घूम आया था और दो मृगशावक मन्त्रमुग्ध-से झाड़ियों में से निकलकर उनकी ओर देखते रह गए थे, वाङ्चू एक पीपल के पेड़ के नीचे घण्टों नतमस्तक बैठा रहा था, यहाँ तक कि उसके कथनानुसार उसके मस्तक में अस्फुट से वाक्य गूँजने लगे थे और उसे लगा था, जैसे महाप्राण का पहला प्रवचन सुन रहा है। वह इस भक्तिपूर्ण कल्पना में इतना गहरा डूब गया था कि सारनाथ में ही रहने लगा था। गंगा की धार को दसियों शताब्दियों के धुँधलके में पावन जलप्रवाह के रूप में देखता। जब श्रीनगर में आया था, बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियों की ओर देखते हुए अक्सर मुझसे कहता—वह रास्ता ल्हासा को जाता है ना, उसी रास्ते बौद्ध ग्रन्थ तिब्बत में भेजे गए थे। वह उस पर्वतमाला को भी पुण्य-पावन मानता था, क्योंकि उस पर बिछी पगडण्डियों के रास्ते बौद्ध भिक्षु तिब्बत की ओर गए थे।
वाङ्चू कुछ वर्षों पहले वृद्ध प्रोफेसर तान-शान के साथ भारत आया था। कुछ दिनों तक तो वह उन्हीं के साथ रहा और हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन करता रहा, फिर प्रोफेसर शान चीन लौट आए और वह यहीं बना रहा और किसी बौद्ध सोसाइटी से अनुदान प्राप्त कर सारनाथ में आकर बैठ गया। भावुक, काव्यमयी प्रकृति का जीव, जो प्राचीनता के मनमोहक वातावरण में विचरते रहना चाहता था। वह यहाँ तथ्यों की खोज करने नहीं आया था। वह तो बोधिसत्त्वों की मूर्तियों को देखकर गदगद होने आया था। महीने-भर से संग्रहालयों के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि बौद्ध धर्म की किस शिक्षा से उसे सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है। न तो वह किसी तथ्य को पाकर उत्साह से खिल उठता, न उसे कोई संशय परेशान करता। वह भक्त अधिक और जिज्ञासू कम था।
मुझे याद नहीं कि उसने हमारे साथ कभी खुलकर बात की हो, या किसी विषय पर अपना मत पेश किया हो। उन दिनों मेरे और मेरे दोस्तों के बीच घण्टों बहसें चला करतीं, कभी देश की राजनीति के बारे में, कभी धर्म के बारे में, लेकिन वाङ्चू इनमें कभी भाग नहीं लेता था। वह सारा वक्त धीमे-धीमे मुस्कराता रहता और कमरे के एक कोने में दुबककर बैठा रहता। उन दिनों देश में वलवलों का सैलाब-सा उठ रहा था। स्वतन्त्रता आन्दोलन जोरों पर था और हमारे बीच उसी की चर्चा रहती—कांग्रेस कौन-सी नीति अपनाएगी, आन्दोलन कौन-सा रुख पकड़ेगा। क्रियात्मक स्तर पर तो हम लोग कुछ करते-कराते नहीं थे, लेकिन भावनात्मक स्तर पर उसके साथ बहुत कुछ जुड़े हुए थे। इस पर वाङ्चू की तटस्थता कभी हमें अखरने लगती, तो कभी अचम्भे में डाल देती। वह हमारे देश की ही गतिविधि के बारे में नहीं, अपने देश की गतिविधि में भी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं लेता था। उसके अपने देश के बारे में भी पूछो, तो मुस्कराता सिर हिलाता रहता था।
कुछ दिनों से श्रीनगर की हवा भी बदली हुई थी। कुछ मास पहले यहाँ गोली चली थी। कश्मीर के लोग महाराजा के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और अब कुछ दिनों से शहर में उत्तेजना पाई जाती थी। नेहरू जी श्रीनगर आने वाले थे और उनका स्वागत करने के लिए नगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। आज ही दोपहर को नेहरू जी श्रीनगर पहुँच रहे हैं। नदी के रास्ते नावों के जुलूस की शक्ल में उन्हें लाने की योजना थी और इसी कारण मैं वाङ्चू को खोजता हुआ उस ओर आ निकला था।
हम घर की ओर बढ़े जा रहे थे, जब सहसा वाङ्चू ठिठककर खड़ा हो गया।
‘‘क्या मेरा जाना बहुत जरूरी है ? जैसा तुम कहो...’’
मुझे धक्का-सा लगा। ऐसे समय में, जब लाखों लोग नेहरू जी के स्वागत के लिए इकट्ठे हो रहे थे, वाङ्चू का यह कहना कि अगर वह साथ में न जाए तो, कैसा रहे, मुझे सचमुच बुरा लगा। लेकिन फिर स्वयं ही कुछ सोचकर उसने अपने आग्रह को दोहराया नहीं और हम घर की ओर साथ-साथ जाने लगे।
कुछ देर बाद हब्बाकदल के पुल के निकट लाखों की भीड़ में हम लोग खड़े थे—मैं वाङ्चू तथा मेरे दो-तीन मित्र। चारों ओर, जहाँ तक नजर जाती, लोग ही लोग थे—मकानों की छतों, पुल पर, नदी के ढलवाँ किनारों पर। मैं बार-बार कनखियों से वाङ्चू के चेहरे की ओर देख रहा था कि उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है, कि हमारे दिल में उठने वाले वलवलों का उस पर क्या असर हुआ है। यों भी यह मेरी आदत-सी बन गई है, जब भी कोई विदेशी साथ में हो, मैं उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ कि हमारे रीति-रिवाजों, हमारे जीवनयापन के बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। वाङ्चू अधमुँदी आँखों से सामने का दृश्य देखे जा रहा था। जिस समय नेहरू जी की नाव सामने आई, तो जैसे मकानों की छतें भी हिल उठीं। राजहंस की शक्ल की सफेद नाव में नेहरू जी स्थानीय नेताओं के साथ खड़े हाथ हिला-हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। और हवा में फूल ही फूल बिखर गए। मैंने पलटकर वाङ्चू के चेहरे की ओर देखा। वह पहले ही की तरह निश्चेष्ट-सा सामने का दृश्य देखे जा रहा था।
नदी के किनारे, लालमण्डी की सड़क पर धीरे-धीरे डोलता-सा चला आ रहा था। धूसर रंग का चोगा पहने था और दूर से लगता था कि बौद्ध भिक्षुओं की ही भाँति उसका सिर भी घुटा हुआ है। पीछे शंकराचार्य की ऊँची पहाड़ी थी और ऊपर स्वच्छ नीला आकाश। सड़क के दोनों ओर ऊँचे-ऊँचे सफेदे के पेड़ों की कतारें। क्षण-भर के लिए मुझे लगा, जैसे वाङ्चू इतिहास के पन्नों पर से उतर कर आ गया है। प्राचीन काल में इसी भाँति देश-विदेश से आने वाले चीवरधारी भिक्षु पहाड़ों और घाटियों को लाँघकर भारत में आया करते होंगे। अतीत के ऐसे ही रोमांचकारी धुँधलके में मुझे वाङ्चू भी चलता हुआ नजर आया। जब से वह श्रीनगर में आया था, बौद्ध विहारों के खंडहरों और संग्रहालयों में घूम रहा था। इस समय भी वह लालमण्डी के संग्रहालय में से निकलकर आ रहा था, जहाँ बौद्धकाल के अनेक अवशेष रखे हैं। उसकी मनःस्थिति को देखते हुए वह सचमुच ही वर्तमान से कटकर अतीत के ही किसी कालखण्ड में विचर रहा था।
‘‘बोधिसत्त्वों से भेंट हो गई ?’’ पास आने पर मैंने चुटकी ली।
वह मुस्करा दिया, हल्की टेढ़ी-सी मुस्कान, जिसे मेरी मौसेरी बहन डेढ़ दाँत की मुस्कान कहा करती थी, क्योंकि मुस्कराते वक्त वाङ्चू का ऊपर का होंठ केवल एक ओर से थोड़ा-सा ऊपर उठता था।
‘‘संग्रहालय के बाहर बहुत-सी मूर्तियाँ रखी हैं। मैं वही देखता रहा।’’ उसने धीमे से कहा, फिर वह सहसा भावुक होकर बोला, ‘‘एक मूर्ति के केवल पैर ही पैर बचे हैं....’’
मैंने सोचा, आगे कुछ कहेगा, परन्तु वह इतना भावविह्वल हो उठा था कि उसका गला रुँध गया और उसके लिए बोलना असम्भव हो गया।
हम एक साथ घर की ओर लौटने लगे।
‘‘महाप्राण के भी पैर ही पहले दिखाए जाते हैं।’’ उसने काँपती-सी आवाज में कहा और अपना हाथ मेरी कोहनी पर रख दिया। उसके हाथ का हल्का-सा कम्पन धड़कते दिल की तरह महसूस हो रहा था।
‘‘आरम्भ में महाप्राण की मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती थीं ना ! तुम तो जानते हो, पहले स्तूप के नीचे केवल पैर ही दिखाए जाते थे। मूर्तियाँ तो बाद में बनाई जाने लगी थीं।’’
जाहिर है, बोधिसत्त्व के पैर देखकर उसे महाप्राण के पैर याद आए थे और वह भावुक हो उठा था। कुछ पता नहीं चलता था, कौन-सी बात किस वक्त वाङ्चू को पुलकाने लगे, किस वक्त वह गदगद होने लगे।
‘‘तुमने बहुत देर कर दी। सभी लोग तुम्हारा इन्तजार कर रहे हैं। मैं चिनारों के नीचे भी तुम्हें खोज आया हूँ।’’ मैंने कहा।
‘‘मैं संग्रहालय में था...’’
‘‘वह तो ठीक है, पर दो बजे तक हमें हब्बाकदल पहुँच जाना चाहिए, वरना जाने का कोई लाभ नहीं।’’
उसने छोटे-छोटे झटकों के साथ तीन बार सिर हिलाया और कदम बढ़ा दिए।
वाङ्चू भारत में मतवाला घूम रहा था। वह महाप्राण के जन्म स्थान लुम्बिनी की यात्रा नंगे पाँव कर चुका था, सारा रास्ता हाथ जोड़े हुए। जिस-जिस दिशा में महाप्राण के चरण उठे थे, वाङ्चू मन्त्रमुग्ध-सा उसी-उसी दिशा में घूम आया था और दो मृगशावक मन्त्रमुग्ध-से झाड़ियों में से निकलकर उनकी ओर देखते रह गए थे, वाङ्चू एक पीपल के पेड़ के नीचे घण्टों नतमस्तक बैठा रहा था, यहाँ तक कि उसके कथनानुसार उसके मस्तक में अस्फुट से वाक्य गूँजने लगे थे और उसे लगा था, जैसे महाप्राण का पहला प्रवचन सुन रहा है। वह इस भक्तिपूर्ण कल्पना में इतना गहरा डूब गया था कि सारनाथ में ही रहने लगा था। गंगा की धार को दसियों शताब्दियों के धुँधलके में पावन जलप्रवाह के रूप में देखता। जब श्रीनगर में आया था, बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियों की ओर देखते हुए अक्सर मुझसे कहता—वह रास्ता ल्हासा को जाता है ना, उसी रास्ते बौद्ध ग्रन्थ तिब्बत में भेजे गए थे। वह उस पर्वतमाला को भी पुण्य-पावन मानता था, क्योंकि उस पर बिछी पगडण्डियों के रास्ते बौद्ध भिक्षु तिब्बत की ओर गए थे।
वाङ्चू कुछ वर्षों पहले वृद्ध प्रोफेसर तान-शान के साथ भारत आया था। कुछ दिनों तक तो वह उन्हीं के साथ रहा और हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन करता रहा, फिर प्रोफेसर शान चीन लौट आए और वह यहीं बना रहा और किसी बौद्ध सोसाइटी से अनुदान प्राप्त कर सारनाथ में आकर बैठ गया। भावुक, काव्यमयी प्रकृति का जीव, जो प्राचीनता के मनमोहक वातावरण में विचरते रहना चाहता था। वह यहाँ तथ्यों की खोज करने नहीं आया था। वह तो बोधिसत्त्वों की मूर्तियों को देखकर गदगद होने आया था। महीने-भर से संग्रहालयों के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि बौद्ध धर्म की किस शिक्षा से उसे सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है। न तो वह किसी तथ्य को पाकर उत्साह से खिल उठता, न उसे कोई संशय परेशान करता। वह भक्त अधिक और जिज्ञासू कम था।
मुझे याद नहीं कि उसने हमारे साथ कभी खुलकर बात की हो, या किसी विषय पर अपना मत पेश किया हो। उन दिनों मेरे और मेरे दोस्तों के बीच घण्टों बहसें चला करतीं, कभी देश की राजनीति के बारे में, कभी धर्म के बारे में, लेकिन वाङ्चू इनमें कभी भाग नहीं लेता था। वह सारा वक्त धीमे-धीमे मुस्कराता रहता और कमरे के एक कोने में दुबककर बैठा रहता। उन दिनों देश में वलवलों का सैलाब-सा उठ रहा था। स्वतन्त्रता आन्दोलन जोरों पर था और हमारे बीच उसी की चर्चा रहती—कांग्रेस कौन-सी नीति अपनाएगी, आन्दोलन कौन-सा रुख पकड़ेगा। क्रियात्मक स्तर पर तो हम लोग कुछ करते-कराते नहीं थे, लेकिन भावनात्मक स्तर पर उसके साथ बहुत कुछ जुड़े हुए थे। इस पर वाङ्चू की तटस्थता कभी हमें अखरने लगती, तो कभी अचम्भे में डाल देती। वह हमारे देश की ही गतिविधि के बारे में नहीं, अपने देश की गतिविधि में भी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं लेता था। उसके अपने देश के बारे में भी पूछो, तो मुस्कराता सिर हिलाता रहता था।
कुछ दिनों से श्रीनगर की हवा भी बदली हुई थी। कुछ मास पहले यहाँ गोली चली थी। कश्मीर के लोग महाराजा के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और अब कुछ दिनों से शहर में उत्तेजना पाई जाती थी। नेहरू जी श्रीनगर आने वाले थे और उनका स्वागत करने के लिए नगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। आज ही दोपहर को नेहरू जी श्रीनगर पहुँच रहे हैं। नदी के रास्ते नावों के जुलूस की शक्ल में उन्हें लाने की योजना थी और इसी कारण मैं वाङ्चू को खोजता हुआ उस ओर आ निकला था।
हम घर की ओर बढ़े जा रहे थे, जब सहसा वाङ्चू ठिठककर खड़ा हो गया।
‘‘क्या मेरा जाना बहुत जरूरी है ? जैसा तुम कहो...’’
मुझे धक्का-सा लगा। ऐसे समय में, जब लाखों लोग नेहरू जी के स्वागत के लिए इकट्ठे हो रहे थे, वाङ्चू का यह कहना कि अगर वह साथ में न जाए तो, कैसा रहे, मुझे सचमुच बुरा लगा। लेकिन फिर स्वयं ही कुछ सोचकर उसने अपने आग्रह को दोहराया नहीं और हम घर की ओर साथ-साथ जाने लगे।
कुछ देर बाद हब्बाकदल के पुल के निकट लाखों की भीड़ में हम लोग खड़े थे—मैं वाङ्चू तथा मेरे दो-तीन मित्र। चारों ओर, जहाँ तक नजर जाती, लोग ही लोग थे—मकानों की छतों, पुल पर, नदी के ढलवाँ किनारों पर। मैं बार-बार कनखियों से वाङ्चू के चेहरे की ओर देख रहा था कि उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है, कि हमारे दिल में उठने वाले वलवलों का उस पर क्या असर हुआ है। यों भी यह मेरी आदत-सी बन गई है, जब भी कोई विदेशी साथ में हो, मैं उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ कि हमारे रीति-रिवाजों, हमारे जीवनयापन के बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। वाङ्चू अधमुँदी आँखों से सामने का दृश्य देखे जा रहा था। जिस समय नेहरू जी की नाव सामने आई, तो जैसे मकानों की छतें भी हिल उठीं। राजहंस की शक्ल की सफेद नाव में नेहरू जी स्थानीय नेताओं के साथ खड़े हाथ हिला-हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। और हवा में फूल ही फूल बिखर गए। मैंने पलटकर वाङ्चू के चेहरे की ओर देखा। वह पहले ही की तरह निश्चेष्ट-सा सामने का दृश्य देखे जा रहा था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i 






_m.jpg)

_s.jpg)