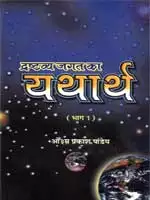|
भारतीय जीवन और दर्शन >> द्रष्टव्य जगत का यथार्थ - भाग 2 द्रष्टव्य जगत का यथार्थ - भाग 2ओम प्रकाश पांडेय
|
151 पाठक हैं |
|||||||
भारत की कालजयी संस्कृति की निरंतता एवं उसकी पृष्ठभूमि का अभिनव वेदांत....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘दृष्टव्य जगत का यथार्थ’ नामक ग्रंथ दो खण्डो में प्रस्तुत
किया जा रहा है। इनमें पूर्ववर्ती रचनाकारों की श्रृंखला की एक नवीन कड़ी
के रूप में सँजोने के साथ-साथ इनमें उल्लिखित प्राचीन संदर्भों को आधुनिक
परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का यथासंभव प्रयत्न किया गया है। यथार्थ
का तात्पर्य दृष्टि-सापेक्ष वास्तविकताओं से होता है।
‘दृष्टव्य जगत का यथार्थ’ एक अदभुत एवं विलक्षण उपक्रम है। पुरातन साहित्य, के विस्तृत कानन में प्रविष्ट होकर विद्वान लेखक ने संदर्भों को जोड़ने एवं उनकी व्याख्या करने में अपनी प्रतिभा का प्रमाण प्रस्तुत किया है।
प्रस्तुत ग्रन्थ ‘दृष्टव्य जगत का यथार्थ’ भारत की कालजयी संस्कृति की निरंतरता एवं उसकी पृष्टभूमि का अभिनव वेदांत है। इसकी पृष्ठभूमि में और उसकी व्याख्याओं में एक चमत्कार है, एक सम्मोहन है, एक सदाचेतन अंतर्धारा है, जो हमारे भारतीय उत्स को अभिसंचित करते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में समाविष्ट भारतीय साहित्य दर्शन, पुराण, परम्परा, भूगोल, इतिहास एवं संस्कृत के अगणित संदर्भ और प्रमाण विश्वकोश की तरह ही हैं।
चूँकि योग्यतम ही जीवन संग्राम में बचा रह पाता है, अतः आपके अन्दर का स्वत्व यदि इस पुस्तक के पढ़ने से जाग्रत हो सके तो लेखक का यह सत्प्रयास सफल हो जायेगा। ‘दृष्टव्य जगत् का यथार्थ’ अपने तरह का सर्वथा, ज्ञानपरक, खोजपरक एवं संग्रहणीय ग्रन्थ है।
‘दृष्टव्य जगत का यथार्थ’ एक अदभुत एवं विलक्षण उपक्रम है। पुरातन साहित्य, के विस्तृत कानन में प्रविष्ट होकर विद्वान लेखक ने संदर्भों को जोड़ने एवं उनकी व्याख्या करने में अपनी प्रतिभा का प्रमाण प्रस्तुत किया है।
प्रस्तुत ग्रन्थ ‘दृष्टव्य जगत का यथार्थ’ भारत की कालजयी संस्कृति की निरंतरता एवं उसकी पृष्टभूमि का अभिनव वेदांत है। इसकी पृष्ठभूमि में और उसकी व्याख्याओं में एक चमत्कार है, एक सम्मोहन है, एक सदाचेतन अंतर्धारा है, जो हमारे भारतीय उत्स को अभिसंचित करते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में समाविष्ट भारतीय साहित्य दर्शन, पुराण, परम्परा, भूगोल, इतिहास एवं संस्कृत के अगणित संदर्भ और प्रमाण विश्वकोश की तरह ही हैं।
चूँकि योग्यतम ही जीवन संग्राम में बचा रह पाता है, अतः आपके अन्दर का स्वत्व यदि इस पुस्तक के पढ़ने से जाग्रत हो सके तो लेखक का यह सत्प्रयास सफल हो जायेगा। ‘दृष्टव्य जगत् का यथार्थ’ अपने तरह का सर्वथा, ज्ञानपरक, खोजपरक एवं संग्रहणीय ग्रन्थ है।
कामना
रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां,
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव।।
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव।।
जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ भिन्न-भिन्न स्रोतों से निकलकर टेढ़े-मेढ़े
रास्ते को अपनाते हुए अंतत: समुद्र में एकाएक हो जाती हैं, उसी प्रकार
विभिन्न विचारों व आस्थाओं को अपनानेवाले लोग विविध उपायों द्वारा सत्य के
एकमात्र छोर तक पहुँचने का ही प्रयास करते हैं।
यही कारण है कि-
यही कारण है कि-
अयं निज: परोवेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितनान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।
उदारचरितनान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।
विशाल हृदयवाले गुणीजन संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं, जबकि
संकीर्ण विचारवाले मनुष्य अपने-पराए के भेद तक ही सीमित रहते हैं।
अत:-
अत:-
भद्रम् इद् भद्रा कृणवत्सरस्वती,
अकवारी चेतति वाजिनीवती।।
अकवारी चेतति वाजिनीवती।।
कल्याणकारिणी विद्या हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करे एवं कुत्सित
विचारों को नष्ट करनेवाली प्रज्ञा इसके लिए हमें प्रबुद्ध करती रहे।
ताकि-
ताकि-
सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुखभाग्भवेत्।।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुखभाग्भवेत्।।
सभी सुखी रहें, सभी निर्मल जन सुरक्षित रहें, सभी कल्याण की कामना से
एक-दूसरे को देखें तथा कोई किसी प्रकार से दु:खी न रहे।
आमुख
‘दृष्टव्य जगत् का यथार्थ’ एक अद्भुत और विलक्षण
उपक्रम है।
कोई अदृश्य शक्ति है जो श्री ओम प्रकाश पांडेय के अनुसंधान की दुस्तर
वीथियों को आलोकित करती है। पुरातन साहित्य के सुविशाल कानन में प्रविष्ट
होकर विद्वान लेखक ने संदर्भों को जोड़ने एवं उनकी व्याख्या करने में अपनी
अद्वितीय प्रतिभा का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ भारत की कालजयी
संस्कृति की निरंतरता एवं उसकी पृष्ठभूमि का अभिनव वेदांत है। इस
पृष्ठभूमि में और उसकी व्याख्याओं में एक चमत्कार है, एक सम्मोहन है,
एकसदा चेतन अंतर्धारा है, जो हमारे भारतीय उत्स को अभिसिंचित करते हैं। इस
ग्रंथ में समाविष्ट भारतीय साहित्य, दर्शन, पुराण, परंपरा, भूगोल, इतिहास
एवं संस्कृत के अगणित संदर्भ और साक्ष्य एक विश्वकोश की तरह प्रतीत होते
हैं, जिनमें विद्वान लेखक की श्रमसाध्य कल्पना का इंद्रधनुष हमारी अस्मिता
के आकाश की मनोरम छवि को प्रतिभासित करती है।
(डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी)
पूर्वपीठिका
विश्व-इतिहास के अध्ययन से यह उद्घाटित होता है कि सिंधु, सुमेरियन,
बेबीलोनियन, असीरियन, कैल्डियन, ईजिष्टियन, यूनानी, पर्सियन, आर्यंस,
मयांस आदि प्राचीन सभ्यताओं के उद्भव-स्थल कर्क रेखा के उत्तरी क्षेत्र
विशेष ही रहे थे। यही कारण रहा था कि देवयुगीन घटनाओं के साथ अत्रि,
पुलस्त्य, यम, मत्स्य समेत प्रलय आदि प्राचीन घटनाओं का वर्णन इन सभ्यताओं
में समान रूप से पाया जाता है। गाथाओं के अतिरिक्त भाषाई स्तर पर भी इनमें
आश्चर्यजनक समानताएँ रही थीं।
वैदिक ‘मित्र’ के अनुरूप जेंद अवेस्ता में मिथ्र, वायु के लिए वाध्यु, मंत्र के लिए मंथ्र, आहुति के लिए आजुइत, सोम के लिए ह्ओम यम के लिए यिम, गंधर्व के लिए गंदरेव जैसे समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, वही वरुण के लिए सुमेरु भाषा में उरुनिन्ना, महाशनि के लिए मेस्सनिपाद, इलविल के लिए एलुलु, हिरण्यपुर के लिए निघुर, और्व के लिए उरु-बऊ, बलि के लिए बेल, विरोचन के लिए वियोर, हिरण्यकशिपु के लिए जियस, नरसिंह के लिए नरमसिन, मारीच के लिए मारीक का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त दृष्टांत यह स्पष्ट करते हैं कि इन विभिन्न सभ्यताओं के जनक एक ही कुल-परिवार से संबंधित रहे थे, किंतु कालक्रम में हुए परिवर्तनों के कारण विकसित सभ्यताओं में इनका स्वरूप भी शनै:-शनै: बदलता चला गया। भारतीय वाङ्मम के अनुसार मारीचि-कश्यप व तेरह महिमामयी दक्ष-दुहिताओं के वंशधर रहे दैत्य, देव, दानव यक्ष, गंधर्व, वैनतेय, काद्रवेय, कालकेय, किन्नर आदि ही भारत के प्रसिद्ध सूर्यवंश (रामादि), चंद्रवंश (कौरव-पांडव-यदु आदि) व नागवंश (तक्षक-भारशिव नागादि) सहित सुमेरियन, असीरियन, मयांस इत्यादि परवर्ती सभ्यताओं के यशस्वी पूर्वज ही रहे थे। कालांतर में इन्हीं सभ्यताओं के गर्भ से कार्पेथोडैन्यूबीयन, स्कैंडेनेह्वियन, एट्रुस्कन, गैलिक, केल्टिक, डुईड, पिलेसगियंस, मेडिज, अरमेह, कूर्द, उज्बेग, डच, आर्गिनोरिस, तुर्क, हिब्रु आदि नूतन जातियों समेत आर्य आर्येंस का अस्तित्व उभरकर सामने आया।
हिम-गुफाओं के विश्लेषण पर आधारित निष्कर्षों के अनुसार आज से लगभग 20 हजार वर्ष पूर्व प्रारंभ हुए अंतर्हिम युगों की अनुकूल परिस्थितियों में मरीचि कुल के यशस्वी पुरुष रहे कश्यप, भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित सुमेरु अंचल के क्षीरसागर (कश्यप सागर) के तटवर्ती क्षेत्र के एक रमणीय स्थान पर अपने आश्रम को स्थापित किया था। इन्हीं कश्यप को प्राचेतस-दक्ष ने अपनी तेरह कन्याएँ सौंपी थीं। महर्षि कश्यप को इन तेरह दक्ष-दुहिताओं से अनेक संतानें हुईं, जो अलग-अलग माताओं के गर्भ से जनमने के कारण पिता के बजाय संबद्ध माताओं के नाम से ही पहचानी गईं। हिमखंडों के पिघलने से उपलब्ध हुए काकेशियस रीजन के क्षेत्रों को अपने आधिपत्य में लेते हुए कश्यप के इन पुत्रों ने उत्तरी ईरान से लेकर भूमध्यसागर के तटीय क्षेत्रों तक अपनी सुविधा व सामर्थ्य के अनुसार अलग-अलग उपनिवेशों की स्थापना कर ली। पैतृक संपत्ति के असंतुलित विभाजन के कारण एक ही प्रजापति (कश्यप) के संतान रहे दैत्य, देव, दानव आदि दायाद बंधुओं (उभये प्रजापत्या देव दैत्य दानवा:) के समूहों में शनै:-शनै: वैमनस्यता के बीज अंकुरित होते चले गए और स्थितियों के कारण अंतत: ये एक-दूसरे के घोर शत्रु बन गए। गुटों में विभाजित दैत्यों और देवों के संगठनों (देवा: पितरो मनुष्य नागाऽन्यत आसन् असुरा रक्षांसि पिशाचा अन्यत:-जै.ब्रा.) के मध्य आपसी युद्ध की यह परंपरा 300 वर्षों तक अनवरत चलती रही थी। (अथ देवासुरं युद्धमभूद्धर्षशतत्रयम्-मत्स्य पुराण-24/37)। इस प्रकार विविध कारणों से हुए इन बारह विश्वयुद्धों को संस्कृत वाङ्मय में ‘देवासुर संग्रामों’ के रूप में चिह्नित किया गया है।
ज्येष्ठ होने के कारण पिता कश्यप के स्वाभाविक उत्तराधिकारी रहे दिति-पुत्र हिरण्यकशिपु ने हंगरी व रोमानिया के मध्य स्थित एक रमणीय स्थान पर ‘हिरण्यपुर’ नामक राजधानी को स्थापित कर ‘दैत्यवंश’ की नींव डाली थी (हिरण्य नाम पुरी रम्या कशिपुर्दैत्य तिष्ठतः)। संभवतः कश्यप सागर के तटवर्ती क्षेत्रों, जिसे अब औक्सस या पारदिया के नाम से चिह्नित किया जाता है, में स्थित सुवर्ण खदानों पर आधिपत्य रखने के कारण हिरण्यकशिपु शीघ्र ही समृद्धशाली हो गया था। इसी के साथ अपने अति पराक्रमी अनुज हिरण्याक्ष के सहयोग से निकटवर्ती क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके उसने दैत्य-साम्राज्य का समुचित विस्तार भी कर लिया। इन अभियानों में दानवों, कालिकेय आदि मौसेरे भाइयों का अनवरत सहयोग भी उसे मिलता रहा था। उधर आधुनिक ईरान के ‘एलम’ क्षेत्र में ‘सुषानगरी’ (सूशन) नामक राजधानी में अधिष्ठित हुए अदिति के पुत्रों में श्रेष्ठ रहे वरुण के समन्वयवादी नीतियों के परिणामस्वरूप असुर वाराह आदि प्राचीनतम जातियों के अतिरिक्त नागादि का रुझान आदित्यों के ही प्रति बना रहा था। हालाँकि वरुण के वर्चस्व तक आदित्यों तथा दैत्यों में भी किसी प्रकार के गंभीर अनबन का प्रसंग उपस्थित नहीं हो पाया था, फिर भी सत्ता-वर्चस्व को लेकर दोनों गुट एक-दूसरे के प्रति शंकालू अवश्य ही बने रहे थे।
कालांतर में वरुण-अनुज इंद्र द्वारा अमरावती में ‘देव’ नामक नई सभ्यता को विकसित करने तथा आदित्यों में कनिष्ठ रहे विष्णु के दैत्य-विरोधी नीतियों का खुला समर्थन करने के कारण दैत्यों तथा देव रूपी आदित्यों के नए संस्करण के मध्य आपसी मतभेद की परंपरागत खाई स्पष्टत: गहरी होती चली गई। इसी मध्य दैत्यपति हिरण्यकशिपु के वरद्हस्त तथा दानवों के सहयोग से बेबीलोन का अधिपति बन चुके महाबली हिरण्याक्ष ने आदित्यों के हितैषी रहे वाराहों के केतुमाल (कोला पैनिन्सुला,यानी नार्वे) का भी बलात् अधिग्रहण कर लिया था। कालक्रम में हुए परिवर्तनों के कारण यहां की आदिम जातियों को कभी कोला-वाराह और अब उसी के प्रतीकात्मक कोल्ट-कैल्ट के नाम से जाना जाता है। हिरण्याक्ष द्वारा बलपूर्वक बंधक बनाए जाने से यह द्वीप तथा यहाँ के निवासियों का संपर्क विश्व के अन्य भागों, विशेषकर आदित्यों से लगभग कटकर रह गया था। संपर्क विहीन होने के कारण समुद्र की अथाह जलराशि में लगभग विलीन से होकर रह गए यहां के निवासियों को हिरण्याक्ष की दासता से मुक्त कराने के उद्देश्य से आदित्य-विष्णु ने समुद्र-गर्भ के अगम किंतु सुरक्षित जलमार्ग द्वारा इस क्षेत्र में प्रवेश कर वाराहों को दैत्यों के विरुद्ध संगठित करना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश समुद्र-स्नान के एक उपयुक्त अवसर पर हिरण्याक्ष को एकाकी पाकर गोताखोरी में दक्ष रहे वाराहों के कुछ उत्साही युवकों ने विष्णु के संकेत पर अगम जलराशि के मध्य ले जाकर इसे डुबोकर मार डाला। इस तरह विष्णु के अथक प्रयासों से हिरण्याक्ष का अंत करके वाराह जहाँ दैत्यों के चंगुल से मुक्त हो गए, वहीं हिरण्याक्ष की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए आदित्य विवस्वान के पराक्रमी पौत्र नृग ने इसके राज्य (आधुनिक बेबीलोनिया) पर कब्जा करके दैत्य-वर्चस्व को बहुत हद तक संकुचित करके रख दिया।
इधर सम्राट हिरण्यकशिपु द्वारा दैत्यों से कनिष्ठ रहे देवों (कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुरा:-शतपथ ब्राह्मण-14.4.1.1) के पैतृक राज्य विभाजन की माँगों को ठुकराए जाने के कारण (असुराणां वा इयं पृथिव्यासीत् ते देवा अब्रुवन दत्तनोऽस्या इति-काठक संहिता 31-/8) दैत्यों देवों में तीन विकट देवासुर संग्राम हो चुके थे। देव-पक्षीय परिणामजनित इन युद्धों के उपरांत भी देवताओं के मार्ग में हिरण्यकशिपु एक अवरोधक की भाँति ही बना रहा था। अत: इस बाधा के समूल निस्तारण के लिए देवहितैषी विष्णु ने देवर्षि नारद के माध्यम से गुरुकुल में दीक्षा ले रहे हिरण्यकशिपु के ज्येष्ठ पुत्र प्रह्लाद को पिता के विरुद्ध बरगलाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। विष्णु के कूट-मंत्रों के प्रभाववश प्रह्लाद यह मानने के लिए विवश हो गया कि हिरण्यकशिपु के दंभी स्वभाव के कारण ही उभय पक्षों में कलह के विषवृक्ष अंकुरित हो रहे हैं, जो प्रकारांतर में दोनों कुलों को विनाओश की काली छाया से ही ढक देंगे।
कुल-उद्धार की क्रांतिकारी भावना से प्रेरित होकर प्रह्लाद ने पिता के विरुद्ध दैत्य समाज को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। दैत्यों के विनाश के लिए संकल्परत रहे विष्णु को हिरण्यकशिपु से मुक्ति के लिए प्रह्लाद द्वारा छेड़ा गया यह अभियान उपयुक्त प्रतीत हुआ। फलत: हिरण्याक्ष के साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर उत्साहित हो रहे युवा नृग को उन्होंने प्रह्लाद से आत्मीयता बढ़ाने तथा मौका पाते ही वृद्ध हिरण्यकशिपु को मार डालने के लिए उद्यत किया। संयोग से रष्ट्र-द्रोह के अभियोग में प्रह्लाद को मृत्यु-दंड देने की हिरण्यकशिपु की घोषणा से राजपुरुषों सहित सामान्य जनता में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। गोधूलि के अस्पष्ट प्रकाश का लाभ उठाते हुए वध-स्थल पर छद्मवेष में पहुँचे वैवस्वत मनु के पुत्र नृगदेव ने बघनखे के प्रयोग द्वारा वृद्ध दैत्य सम्राट हिरण्यकशिपु का वध कर डाला (देवारिर्दितिजो वीरों नृसिंह समुपाद्रवत् समुत्पत्य ततस्तीक्ष्णैर्मृगेन्द्रेण महानखै:-विदार्य निहतो युधि मत्स्य पुराण 163/94)। हिरण्यकशिपु के वध से प्राणदान पा चुके प्रह्लाद व उसके शुभेच्छुओं ने नृग के इस अपूर्व पराक्रम से अभिभूत होकर उन्हें ‘नृग-सिंह-देव’ (नृसिंहदेव) की उपाधि से विभूषित कर दिया।
प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता मार्गन मिशन को बेबीलोनिया तथा लुलबी (बगदाद के निकट) के क्षेत्रों में हुई खुदाई से प्राप्त भित्ति चित्रों में नृसिंह को सूर्यांकित ध्वजा लेकर सैन्य-संचालन करते दिखाया गया है। हिरण्यकशिपु के अनुमानित वध-स्थान, अर्थात् सुमना पर्वत (कश्यप सागर के निकट स्थित एलब्रुज पर्वत) क्षेत्र में आज भी अर्ध-सिंह व अर्ध-नर की एक मूर्ति स्थापित है, जिसे यहाँ की पुरानी मान्यताओं में ‘नरमसिन’ कहा जाता रहा है। हिरण्यकशिपु के उपरांत दैत्य-सम्राट बने देव हितैषी प्रह्लाद तथा उसके पुत्र विरोचन के राज्य-कालों में दैत्यों व देवों के मध्य आपसी सौहार्द का भाव बना रहा था और इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए देवों ने अपनी शक्ति को काफी विकसित भी कर दिया था।
प्रह्लाद की देव हितैषी नीतियों का अनुसरण करते हुए उसके पुत्र विरोचन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए देवों के पैतृक राज्य के बँटवारे की लंबित पड़ी माँग को स्वीकार कर लिया। चूँकि कैस्पियन व काला सागरों के मध्य फैले पैतृक राज्य के आर्थिक स्रोत का मुख्य आधार संबंधित समुद्रीय क्षेत्र ही रहे थे, अत: बँटवारे के विचार-विमर्श के लिए आहूत इस गोष्ठी को ‘समुद्र-मंथन’ के नाम से ही चिह्नित किया गया। संभवत: कश्यप सागर (क्षीरसागर) के उत्तरी तट पर स्थित किसी ‘अमृत’ नामक स्थान पर दैत्यों, देवों दानवों, नागों आदि दायाद बंधुओं की यह पंचायत बैठी होगी, जिसकी अध्यक्षता पितामह कश्यप ने की होगी। किंचित् यही कारण रहा होगा कि पौराणिक आख्यानों व चित्रों में समुद्र या अमृतमंथन के इस संदर्भ में देवों व दैत्यों के साथ कच्छप (कश्यप), वासुकि (शेषनाग के बाद नागराज के पद पर अधिष्ठित हुए) व दानवों (राहु-केतु) का भी उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त समुद्र-मंथन के विषय में भविष्य पुराण (67/9) के संदर्भ स्पष्ट रूप से कश्यप सागर (क्षीरसागर) के उत्तर तट में स्थित ‘अमृत’ नामक स्थान की ओर संकेत करते हैं (क्षीरोदस्योत्तरे कूले उदीच्यां दिशि देवता: अमृतं नाम परम् स्थान माहुर्मनीषिण:।
इस पंचायत में अमृत नामक अति समृद्ध स्थान को लेकर उपजे विवादों के कारण दैत्यों और देवों में जो विग्रह हुआ उसे चतुर्थ देवासुर संग्राम के नाम से भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित किया गया है इस युद्ध के पश्चात् विष्णु ने जहाँ दैत्यों के अधिकार में रहे कश्यप सागर (क्षीरसागर) क्षेत्र को हस्तगत कर पूर्वकाल के नारायण द्वारा स्थापित वैकुंठधाम (आधुनिक बैकुड शहर) अपनी राजधानी बना ली थी, वही आदित्य विवस्वान (सूर्य) ने फारस की खाड़ी से उत्तर-पश्चिम के क्षेत्र में ‘सुर’ नामक नगरी बसाकर रहने लगे थे। हिमयुगीन पराकाष्ठा के पश्चात् पिघली बर्फ के कारण क्षीरसागर के जल स्तर में हुई बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप बैकुंठ नामक यह भव्य नगर तदंतर एक टापू में परिवर्तित हो गया। संभवत: यही कराण रहा कि पौराणिक चित्रों में विष्णु के निवास को प्राय: समुद्र के मध्य ही दरशाया गया है। कालांतर में उत्तरी यूरोप में हुए हिम स्खलनों से कैस्पिन सागर के जल स्तर में पुन: हुई बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप द्वारिका नगरी की भाँति अंतत: इसकी भी जल-समाधि हो गई। इस प्रकार काकेशियन क्षेत्र में आदित्यों से निकले वारुणेय, देवो व सुरों का अलग-अलग राज्य स्थापित हो चुका था। इन्हीं सुरों के प्रभाववश उनसे वैमनस्य रखने व विपरीत आचरण करनेवाले दैत्य-दानव आदि इतर कुलों के लिए विवस्वान (सूर्य) के पुत्र रहे मनु द्वारा विकसित सभ्यताओं में इन देव विरोधी शक्तियों के लिए ‘असुर’ का संबोधन किया जाने लगा होगा (न सुरा इति असुरा:) कालांतर में सुरों व असुरों के ये राज्य भाषाई अपभ्रंश के कारण ‘सीरिया’ व ‘असीरिया’ के नाम से विख्यात हुए।
अमृत नामक देवासुर संग्राम के कुछ काल पश्चात् दैत्य-गुरु शुक्राचार्य के पौत्र चंद्र (सोम ) का देव-गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से अवैध संबंध स्थापित हो गया। इस बढ़ते प्रेम-प्रसंग के अतिरेक में चंद्र तारा को भगा ले गया। देव-गुरु की भार्या के साथ किए गए इस अशोभनीय व्यवहार को देवताओं ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। तारा अपहरण कांड के कारण दैत्यों और देवों में हुए इस विग्रह को ‘तारकामय’ नामक पाँचवें देवासुर संग्राम के नाम से जाना गया। इस युद्ध में विरोचन अपने तीनों भ्राताओं सहित तेजस्वी इंद्र के हाथों मारा गया (विरोचनस्तु प्राह्लादिर्नित्यमिन्द्रवधोद्यत: इंद्रेणैव तु विक्रम्य निहितस्तारकामये-मत्स्य पुराण-47/49)। विरोचन वध के पश्चात् चंद्र द्वारा तारा को वापस लौटाए जाने पर ही दोनों पक्षों में संधि स्थापित हो पाई थी। अपहरण काल में गर्भवती हुई तारा को बुध नामक एक पुत्र हुआ, जिसका विवाह मनु-पुत्री इला से हुआ था। इला-बुध के पुत्र एल-पुरुरवा हुए, जिनसे पश्चिमी एशिया का एल तथा भारत का चंद्र वंश चला। चंद्रवंश में ययाति-पुत्र यदु से हैहय व यदु वंश तथा ययति-पुत्र पुरु से पौरव वंश का प्रारंभ हुआ। यदु के कुल में कालजयी कृष्ण व बलराम हुए, जबकि पुरु के कुल में दुष्यंत, भरत, कुरु, प्रतीप, शांतनु के क्रम से कौरव व पांडव हुए। महाभारत युद्ध के पश्चात् जीवित बचे पांडवों के कुल का अंतिम शासक क्षेमक रहा था, जिसका अंत मगध सम्राट महापद्मनंद द्वारा किया गया।
विरोचन के पश्चात् दैत्यपति के पद पर समुद्र-मंथन का नायक रहा, उसका पराक्रमी पुत्र बलि आरूढ़ हुआ। सिंहासनारूढ़ होने के तुरंत पश्चात् पिता की हार का बदला लेते हुए उसने तात्कालिक इंद्र के महिमामयी पद पर अधिष्ठित होकर इस प्रतापी दैत्य ने सातों पातालों समेत पश्चिमी एशिया व यूरोप के सभी राजवंशों को जीतकर ‘त्रिलोकी’ के नाम से विख्यात हुआ (बलिनाऽधिष्ठिते चैव पुरा लोकत्रयेक्रमात्-मस्त्य पुराण-47/36)। बलि एक कुशल योद्धा तथा सफल प्रकाशक होने के साथ-साथ मुक्त हस्त से दान करनेवाला एक उदार नृप भी रहा था। उसकी इस कमजोर नस को भाँपते हुए विष्णु ने देवहित में बलि को उद्यमजनित विजय को पराजय में बदलने के लिए छल का सहारा लिया। धर्मनिष्ठ बलि द्वारा आयोजित एक यज्ञ-अनुष्ठान में विष्णु द्वारा भेजे गए नाटे कद के ‘बटुक’ ने उससे यज्ञ कर्म के लिए तीन पग भूमि दान में माँगी। वामन रूपी उस याचक के इस छुद्र प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करते हुए बलि ने उसे इच्छित स्थान पर भूमि को नापकर अपने अधिकार में लेने की राजाज्ञा जारी कर दी। वामन की इस कूट माँग को देव-षड्यंत्र का एक हिस्सा मानते हुए गुरु शुक्राचार्य ने बलि को समझाना चाहा और अंत में उसके इस दैत्यघाती निर्णय से क्षुब्ध होकर वे शाकद्वीप (अरब) चले गए। यहीं पर शुक्राचार्य ने अपने आराध्य शिव के लिंग को स्थापित कर एक भव्य मंदिर बनवाया था, जो कालांतर में ‘काव्य का मंदिर’ व तदनुरूप ‘काबा’ के नाम से विख्यात हुआ।
इधर बलि के निर्देशानुसार ‘तीन पग भूमि’ के क्रम से अग्निकुंडों को स्थापित करते हुए वामन व उसके सहयोगी दैत्यों के नगरों तथा पुरों को अपने अधिकार में करते चले गए। बलि द्वारा पूछे जाने पर वामन रूपी उस याचक ने तीन पगों का आशय वेद वर्णित ब्रह्म के पदों से (पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादयाभृतं दिवि-ऋ.-10-90-3) करते हुए उसे निरूत्तर कर दिया। अपनी वचनबद्धता के कारण निरुपाय हो चुके बलि को अंततोगत्वा राजमहल तक का त्याग करते हुए बंधु-बांधवों सहित सातों पातालों में से एक रहे सुतल (बलख) के दुरूह क्षेत्र में जाकर आश्रय लेना पड़ा था (सुतलं नाम पातालं त्वमासाद्य मनोरमम् वसासुर ममाऽऽदेशं यथावत्परिपालयन्-मत्स्य पुराण-246/75)। इस प्रकार त्रिलोक विजयी बलि को अपने जीवन का अंतिम समय सुतल स्थित ‘बलसुरा’ (बलि असुर के प्रतीकात्मक नगर जिसको कालांतर में बलख के नाम से जाना जाने लगा) के कष्टमयी वातावरण में बिताना पड़ा था।
प्राकृतिक त्रासदियों के लंबे दौर के पश्चात् इसलाम के दूसरे खलीफा उमर द्वारा 640 ईस्वी में पुन: बसाए गए इस नगर को अब ‘बसरा’ के नाम से जाना जाता है। महाप्राण बलि के पराभव के पश्चात् देवों (पुरंदर आदि इंद्र) का उसके उत्तराधिकारियों से निरंतर सात युद्ध हुए, जो आडीवक, त्रिपूर, अंधक, वृत्रघातक, धात्र हलाहल व कोलाहल नामक ‘देवासुर संग्रामों’ के रूप में विख्यात हुए (संदर्भ-मत्स्य पुराण-47/44.45)। इन देवासुर संग्रामों के पश्चात् दैत्य शक्ति का संपूर्ण विनाश हो गया और देवताओं का वर्चस्व संपूर्ण धरती पर व्याप्त हो गया। हिरण्याक्ष व फिर हिरण्यकशिपु के वधों में सक्रिय भूमिका निभानेवाले वाराहों व नृप-सिंह-देव (नरसिंह देव) तथा पराक्रमी बलि को पदच्युत करानेवाले याचक वामन के कृत्यों के सूत्रधार चूँकि अदिति-पुत्र विष्णु (पौराणिक पुरुष) ही रहे थे, अत: कालांतर में अवतारवाद से प्रभावित ग्रंथों में वाराह, नरसिंह, बामन आदि को विष्णु के ही विभिन्न स्वरूपों के रूप में मान्यताएँ प्रदान करते हुए नाम एकरूपता के कारण इन्हें सृष्टिकर्ता (विष्णु) के अधिभौतिक स्वरूपों (हयग्रीव, कच्छप आदि) की कड़ी से जोड़ दिया गया।
देव-उत्कर्ष के इसी काल में घटित प्रलय की भयंकर त्रासदी के कारण इस क्षेत्र में धन-जन की व्यापक हानि हुई। इस प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप त्रिविष्टप क्षेत्र में रह रहे देवों के कुछ समूहों को छोड़कर पश्चिमी एशिया का उनका साम्राज्य एकदम से नष्टप्राय: हो गया। त्रिविष्टप के इन्हीं देवों में से एक युवक ने आदित्य-कुल के बचे हुए बुजुर्गों के परामर्शों की अनदेखी करते हुए स्वयं को इनका अधिपति घोषित कर दिया। अपने इस निर्णय का विरोध करने पर इस महत्वाकांक्षी देवराट् अद्भुत (इंद्र) ने अपने पिता द्यौस की भी हत्या कर दी थी (संदर्भ-ऋ.4/18)। देवराट् ‘अद्भुत’ नामक इस इंद्र ने त्रिविष्टप स्थित नए देवलोक के पड़ोसी गणों (यक्ष, नाग, गंधर्व आदि) को अपना मित्र बनाते हुए अपने राज्य की प्रतिरोधात्मक क्षमता को सुरक्षित करके देव-वर्चस्व को पुन: प्रतिष्ठापित किया।
देवराट् ‘अद्भुत’ के ही काल में विवस्वान (सूर्य) के पुत्र वैवस्वत मनु मत्स्यों (मछुआरों) के सक्रिय सहयोग से जलप्लावन की त्रासदी से बंधु-बांधवों सहित स्वयं को सुरक्षित बचाते हुए भारत के सिंधु प्रांत में आकर विस्थापित हुए थे। मनु के पलायन कर जाने के बाद उनके विमाता के पुत्र रहे यम ही पितरों के राज्य के स्वामी बने थे। मनु पुत्र इक्ष्वाकु ने भारत के हृदय स्थल (कोशल) में सूर्यवंश की नींव डाली। इसी सूर्यवंश में युवनाश्व, मांधाता, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, भगीरथ, दिलीप, सुदास, रघु, दशरथ, राम आदि प्रतापी सम्राट हुए। इक्ष्वाकु के इस कालजयी कुल का अंतिम शासक सुमित्र हुआ, जिसका वध शैशुनाग वंशी उदायिभद्र के द्वारा किया गया था।
वैदिक ‘मित्र’ के अनुरूप जेंद अवेस्ता में मिथ्र, वायु के लिए वाध्यु, मंत्र के लिए मंथ्र, आहुति के लिए आजुइत, सोम के लिए ह्ओम यम के लिए यिम, गंधर्व के लिए गंदरेव जैसे समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, वही वरुण के लिए सुमेरु भाषा में उरुनिन्ना, महाशनि के लिए मेस्सनिपाद, इलविल के लिए एलुलु, हिरण्यपुर के लिए निघुर, और्व के लिए उरु-बऊ, बलि के लिए बेल, विरोचन के लिए वियोर, हिरण्यकशिपु के लिए जियस, नरसिंह के लिए नरमसिन, मारीच के लिए मारीक का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त दृष्टांत यह स्पष्ट करते हैं कि इन विभिन्न सभ्यताओं के जनक एक ही कुल-परिवार से संबंधित रहे थे, किंतु कालक्रम में हुए परिवर्तनों के कारण विकसित सभ्यताओं में इनका स्वरूप भी शनै:-शनै: बदलता चला गया। भारतीय वाङ्मम के अनुसार मारीचि-कश्यप व तेरह महिमामयी दक्ष-दुहिताओं के वंशधर रहे दैत्य, देव, दानव यक्ष, गंधर्व, वैनतेय, काद्रवेय, कालकेय, किन्नर आदि ही भारत के प्रसिद्ध सूर्यवंश (रामादि), चंद्रवंश (कौरव-पांडव-यदु आदि) व नागवंश (तक्षक-भारशिव नागादि) सहित सुमेरियन, असीरियन, मयांस इत्यादि परवर्ती सभ्यताओं के यशस्वी पूर्वज ही रहे थे। कालांतर में इन्हीं सभ्यताओं के गर्भ से कार्पेथोडैन्यूबीयन, स्कैंडेनेह्वियन, एट्रुस्कन, गैलिक, केल्टिक, डुईड, पिलेसगियंस, मेडिज, अरमेह, कूर्द, उज्बेग, डच, आर्गिनोरिस, तुर्क, हिब्रु आदि नूतन जातियों समेत आर्य आर्येंस का अस्तित्व उभरकर सामने आया।
हिम-गुफाओं के विश्लेषण पर आधारित निष्कर्षों के अनुसार आज से लगभग 20 हजार वर्ष पूर्व प्रारंभ हुए अंतर्हिम युगों की अनुकूल परिस्थितियों में मरीचि कुल के यशस्वी पुरुष रहे कश्यप, भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित सुमेरु अंचल के क्षीरसागर (कश्यप सागर) के तटवर्ती क्षेत्र के एक रमणीय स्थान पर अपने आश्रम को स्थापित किया था। इन्हीं कश्यप को प्राचेतस-दक्ष ने अपनी तेरह कन्याएँ सौंपी थीं। महर्षि कश्यप को इन तेरह दक्ष-दुहिताओं से अनेक संतानें हुईं, जो अलग-अलग माताओं के गर्भ से जनमने के कारण पिता के बजाय संबद्ध माताओं के नाम से ही पहचानी गईं। हिमखंडों के पिघलने से उपलब्ध हुए काकेशियस रीजन के क्षेत्रों को अपने आधिपत्य में लेते हुए कश्यप के इन पुत्रों ने उत्तरी ईरान से लेकर भूमध्यसागर के तटीय क्षेत्रों तक अपनी सुविधा व सामर्थ्य के अनुसार अलग-अलग उपनिवेशों की स्थापना कर ली। पैतृक संपत्ति के असंतुलित विभाजन के कारण एक ही प्रजापति (कश्यप) के संतान रहे दैत्य, देव, दानव आदि दायाद बंधुओं (उभये प्रजापत्या देव दैत्य दानवा:) के समूहों में शनै:-शनै: वैमनस्यता के बीज अंकुरित होते चले गए और स्थितियों के कारण अंतत: ये एक-दूसरे के घोर शत्रु बन गए। गुटों में विभाजित दैत्यों और देवों के संगठनों (देवा: पितरो मनुष्य नागाऽन्यत आसन् असुरा रक्षांसि पिशाचा अन्यत:-जै.ब्रा.) के मध्य आपसी युद्ध की यह परंपरा 300 वर्षों तक अनवरत चलती रही थी। (अथ देवासुरं युद्धमभूद्धर्षशतत्रयम्-मत्स्य पुराण-24/37)। इस प्रकार विविध कारणों से हुए इन बारह विश्वयुद्धों को संस्कृत वाङ्मय में ‘देवासुर संग्रामों’ के रूप में चिह्नित किया गया है।
ज्येष्ठ होने के कारण पिता कश्यप के स्वाभाविक उत्तराधिकारी रहे दिति-पुत्र हिरण्यकशिपु ने हंगरी व रोमानिया के मध्य स्थित एक रमणीय स्थान पर ‘हिरण्यपुर’ नामक राजधानी को स्थापित कर ‘दैत्यवंश’ की नींव डाली थी (हिरण्य नाम पुरी रम्या कशिपुर्दैत्य तिष्ठतः)। संभवतः कश्यप सागर के तटवर्ती क्षेत्रों, जिसे अब औक्सस या पारदिया के नाम से चिह्नित किया जाता है, में स्थित सुवर्ण खदानों पर आधिपत्य रखने के कारण हिरण्यकशिपु शीघ्र ही समृद्धशाली हो गया था। इसी के साथ अपने अति पराक्रमी अनुज हिरण्याक्ष के सहयोग से निकटवर्ती क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके उसने दैत्य-साम्राज्य का समुचित विस्तार भी कर लिया। इन अभियानों में दानवों, कालिकेय आदि मौसेरे भाइयों का अनवरत सहयोग भी उसे मिलता रहा था। उधर आधुनिक ईरान के ‘एलम’ क्षेत्र में ‘सुषानगरी’ (सूशन) नामक राजधानी में अधिष्ठित हुए अदिति के पुत्रों में श्रेष्ठ रहे वरुण के समन्वयवादी नीतियों के परिणामस्वरूप असुर वाराह आदि प्राचीनतम जातियों के अतिरिक्त नागादि का रुझान आदित्यों के ही प्रति बना रहा था। हालाँकि वरुण के वर्चस्व तक आदित्यों तथा दैत्यों में भी किसी प्रकार के गंभीर अनबन का प्रसंग उपस्थित नहीं हो पाया था, फिर भी सत्ता-वर्चस्व को लेकर दोनों गुट एक-दूसरे के प्रति शंकालू अवश्य ही बने रहे थे।
कालांतर में वरुण-अनुज इंद्र द्वारा अमरावती में ‘देव’ नामक नई सभ्यता को विकसित करने तथा आदित्यों में कनिष्ठ रहे विष्णु के दैत्य-विरोधी नीतियों का खुला समर्थन करने के कारण दैत्यों तथा देव रूपी आदित्यों के नए संस्करण के मध्य आपसी मतभेद की परंपरागत खाई स्पष्टत: गहरी होती चली गई। इसी मध्य दैत्यपति हिरण्यकशिपु के वरद्हस्त तथा दानवों के सहयोग से बेबीलोन का अधिपति बन चुके महाबली हिरण्याक्ष ने आदित्यों के हितैषी रहे वाराहों के केतुमाल (कोला पैनिन्सुला,यानी नार्वे) का भी बलात् अधिग्रहण कर लिया था। कालक्रम में हुए परिवर्तनों के कारण यहां की आदिम जातियों को कभी कोला-वाराह और अब उसी के प्रतीकात्मक कोल्ट-कैल्ट के नाम से जाना जाता है। हिरण्याक्ष द्वारा बलपूर्वक बंधक बनाए जाने से यह द्वीप तथा यहाँ के निवासियों का संपर्क विश्व के अन्य भागों, विशेषकर आदित्यों से लगभग कटकर रह गया था। संपर्क विहीन होने के कारण समुद्र की अथाह जलराशि में लगभग विलीन से होकर रह गए यहां के निवासियों को हिरण्याक्ष की दासता से मुक्त कराने के उद्देश्य से आदित्य-विष्णु ने समुद्र-गर्भ के अगम किंतु सुरक्षित जलमार्ग द्वारा इस क्षेत्र में प्रवेश कर वाराहों को दैत्यों के विरुद्ध संगठित करना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश समुद्र-स्नान के एक उपयुक्त अवसर पर हिरण्याक्ष को एकाकी पाकर गोताखोरी में दक्ष रहे वाराहों के कुछ उत्साही युवकों ने विष्णु के संकेत पर अगम जलराशि के मध्य ले जाकर इसे डुबोकर मार डाला। इस तरह विष्णु के अथक प्रयासों से हिरण्याक्ष का अंत करके वाराह जहाँ दैत्यों के चंगुल से मुक्त हो गए, वहीं हिरण्याक्ष की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए आदित्य विवस्वान के पराक्रमी पौत्र नृग ने इसके राज्य (आधुनिक बेबीलोनिया) पर कब्जा करके दैत्य-वर्चस्व को बहुत हद तक संकुचित करके रख दिया।
इधर सम्राट हिरण्यकशिपु द्वारा दैत्यों से कनिष्ठ रहे देवों (कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुरा:-शतपथ ब्राह्मण-14.4.1.1) के पैतृक राज्य विभाजन की माँगों को ठुकराए जाने के कारण (असुराणां वा इयं पृथिव्यासीत् ते देवा अब्रुवन दत्तनोऽस्या इति-काठक संहिता 31-/8) दैत्यों देवों में तीन विकट देवासुर संग्राम हो चुके थे। देव-पक्षीय परिणामजनित इन युद्धों के उपरांत भी देवताओं के मार्ग में हिरण्यकशिपु एक अवरोधक की भाँति ही बना रहा था। अत: इस बाधा के समूल निस्तारण के लिए देवहितैषी विष्णु ने देवर्षि नारद के माध्यम से गुरुकुल में दीक्षा ले रहे हिरण्यकशिपु के ज्येष्ठ पुत्र प्रह्लाद को पिता के विरुद्ध बरगलाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। विष्णु के कूट-मंत्रों के प्रभाववश प्रह्लाद यह मानने के लिए विवश हो गया कि हिरण्यकशिपु के दंभी स्वभाव के कारण ही उभय पक्षों में कलह के विषवृक्ष अंकुरित हो रहे हैं, जो प्रकारांतर में दोनों कुलों को विनाओश की काली छाया से ही ढक देंगे।
कुल-उद्धार की क्रांतिकारी भावना से प्रेरित होकर प्रह्लाद ने पिता के विरुद्ध दैत्य समाज को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। दैत्यों के विनाश के लिए संकल्परत रहे विष्णु को हिरण्यकशिपु से मुक्ति के लिए प्रह्लाद द्वारा छेड़ा गया यह अभियान उपयुक्त प्रतीत हुआ। फलत: हिरण्याक्ष के साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर उत्साहित हो रहे युवा नृग को उन्होंने प्रह्लाद से आत्मीयता बढ़ाने तथा मौका पाते ही वृद्ध हिरण्यकशिपु को मार डालने के लिए उद्यत किया। संयोग से रष्ट्र-द्रोह के अभियोग में प्रह्लाद को मृत्यु-दंड देने की हिरण्यकशिपु की घोषणा से राजपुरुषों सहित सामान्य जनता में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। गोधूलि के अस्पष्ट प्रकाश का लाभ उठाते हुए वध-स्थल पर छद्मवेष में पहुँचे वैवस्वत मनु के पुत्र नृगदेव ने बघनखे के प्रयोग द्वारा वृद्ध दैत्य सम्राट हिरण्यकशिपु का वध कर डाला (देवारिर्दितिजो वीरों नृसिंह समुपाद्रवत् समुत्पत्य ततस्तीक्ष्णैर्मृगेन्द्रेण महानखै:-विदार्य निहतो युधि मत्स्य पुराण 163/94)। हिरण्यकशिपु के वध से प्राणदान पा चुके प्रह्लाद व उसके शुभेच्छुओं ने नृग के इस अपूर्व पराक्रम से अभिभूत होकर उन्हें ‘नृग-सिंह-देव’ (नृसिंहदेव) की उपाधि से विभूषित कर दिया।
प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता मार्गन मिशन को बेबीलोनिया तथा लुलबी (बगदाद के निकट) के क्षेत्रों में हुई खुदाई से प्राप्त भित्ति चित्रों में नृसिंह को सूर्यांकित ध्वजा लेकर सैन्य-संचालन करते दिखाया गया है। हिरण्यकशिपु के अनुमानित वध-स्थान, अर्थात् सुमना पर्वत (कश्यप सागर के निकट स्थित एलब्रुज पर्वत) क्षेत्र में आज भी अर्ध-सिंह व अर्ध-नर की एक मूर्ति स्थापित है, जिसे यहाँ की पुरानी मान्यताओं में ‘नरमसिन’ कहा जाता रहा है। हिरण्यकशिपु के उपरांत दैत्य-सम्राट बने देव हितैषी प्रह्लाद तथा उसके पुत्र विरोचन के राज्य-कालों में दैत्यों व देवों के मध्य आपसी सौहार्द का भाव बना रहा था और इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए देवों ने अपनी शक्ति को काफी विकसित भी कर दिया था।
प्रह्लाद की देव हितैषी नीतियों का अनुसरण करते हुए उसके पुत्र विरोचन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए देवों के पैतृक राज्य के बँटवारे की लंबित पड़ी माँग को स्वीकार कर लिया। चूँकि कैस्पियन व काला सागरों के मध्य फैले पैतृक राज्य के आर्थिक स्रोत का मुख्य आधार संबंधित समुद्रीय क्षेत्र ही रहे थे, अत: बँटवारे के विचार-विमर्श के लिए आहूत इस गोष्ठी को ‘समुद्र-मंथन’ के नाम से ही चिह्नित किया गया। संभवत: कश्यप सागर (क्षीरसागर) के उत्तरी तट पर स्थित किसी ‘अमृत’ नामक स्थान पर दैत्यों, देवों दानवों, नागों आदि दायाद बंधुओं की यह पंचायत बैठी होगी, जिसकी अध्यक्षता पितामह कश्यप ने की होगी। किंचित् यही कारण रहा होगा कि पौराणिक आख्यानों व चित्रों में समुद्र या अमृतमंथन के इस संदर्भ में देवों व दैत्यों के साथ कच्छप (कश्यप), वासुकि (शेषनाग के बाद नागराज के पद पर अधिष्ठित हुए) व दानवों (राहु-केतु) का भी उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त समुद्र-मंथन के विषय में भविष्य पुराण (67/9) के संदर्भ स्पष्ट रूप से कश्यप सागर (क्षीरसागर) के उत्तर तट में स्थित ‘अमृत’ नामक स्थान की ओर संकेत करते हैं (क्षीरोदस्योत्तरे कूले उदीच्यां दिशि देवता: अमृतं नाम परम् स्थान माहुर्मनीषिण:।
इस पंचायत में अमृत नामक अति समृद्ध स्थान को लेकर उपजे विवादों के कारण दैत्यों और देवों में जो विग्रह हुआ उसे चतुर्थ देवासुर संग्राम के नाम से भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित किया गया है इस युद्ध के पश्चात् विष्णु ने जहाँ दैत्यों के अधिकार में रहे कश्यप सागर (क्षीरसागर) क्षेत्र को हस्तगत कर पूर्वकाल के नारायण द्वारा स्थापित वैकुंठधाम (आधुनिक बैकुड शहर) अपनी राजधानी बना ली थी, वही आदित्य विवस्वान (सूर्य) ने फारस की खाड़ी से उत्तर-पश्चिम के क्षेत्र में ‘सुर’ नामक नगरी बसाकर रहने लगे थे। हिमयुगीन पराकाष्ठा के पश्चात् पिघली बर्फ के कारण क्षीरसागर के जल स्तर में हुई बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप बैकुंठ नामक यह भव्य नगर तदंतर एक टापू में परिवर्तित हो गया। संभवत: यही कराण रहा कि पौराणिक चित्रों में विष्णु के निवास को प्राय: समुद्र के मध्य ही दरशाया गया है। कालांतर में उत्तरी यूरोप में हुए हिम स्खलनों से कैस्पिन सागर के जल स्तर में पुन: हुई बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप द्वारिका नगरी की भाँति अंतत: इसकी भी जल-समाधि हो गई। इस प्रकार काकेशियन क्षेत्र में आदित्यों से निकले वारुणेय, देवो व सुरों का अलग-अलग राज्य स्थापित हो चुका था। इन्हीं सुरों के प्रभाववश उनसे वैमनस्य रखने व विपरीत आचरण करनेवाले दैत्य-दानव आदि इतर कुलों के लिए विवस्वान (सूर्य) के पुत्र रहे मनु द्वारा विकसित सभ्यताओं में इन देव विरोधी शक्तियों के लिए ‘असुर’ का संबोधन किया जाने लगा होगा (न सुरा इति असुरा:) कालांतर में सुरों व असुरों के ये राज्य भाषाई अपभ्रंश के कारण ‘सीरिया’ व ‘असीरिया’ के नाम से विख्यात हुए।
अमृत नामक देवासुर संग्राम के कुछ काल पश्चात् दैत्य-गुरु शुक्राचार्य के पौत्र चंद्र (सोम ) का देव-गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से अवैध संबंध स्थापित हो गया। इस बढ़ते प्रेम-प्रसंग के अतिरेक में चंद्र तारा को भगा ले गया। देव-गुरु की भार्या के साथ किए गए इस अशोभनीय व्यवहार को देवताओं ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। तारा अपहरण कांड के कारण दैत्यों और देवों में हुए इस विग्रह को ‘तारकामय’ नामक पाँचवें देवासुर संग्राम के नाम से जाना गया। इस युद्ध में विरोचन अपने तीनों भ्राताओं सहित तेजस्वी इंद्र के हाथों मारा गया (विरोचनस्तु प्राह्लादिर्नित्यमिन्द्रवधोद्यत: इंद्रेणैव तु विक्रम्य निहितस्तारकामये-मत्स्य पुराण-47/49)। विरोचन वध के पश्चात् चंद्र द्वारा तारा को वापस लौटाए जाने पर ही दोनों पक्षों में संधि स्थापित हो पाई थी। अपहरण काल में गर्भवती हुई तारा को बुध नामक एक पुत्र हुआ, जिसका विवाह मनु-पुत्री इला से हुआ था। इला-बुध के पुत्र एल-पुरुरवा हुए, जिनसे पश्चिमी एशिया का एल तथा भारत का चंद्र वंश चला। चंद्रवंश में ययाति-पुत्र यदु से हैहय व यदु वंश तथा ययति-पुत्र पुरु से पौरव वंश का प्रारंभ हुआ। यदु के कुल में कालजयी कृष्ण व बलराम हुए, जबकि पुरु के कुल में दुष्यंत, भरत, कुरु, प्रतीप, शांतनु के क्रम से कौरव व पांडव हुए। महाभारत युद्ध के पश्चात् जीवित बचे पांडवों के कुल का अंतिम शासक क्षेमक रहा था, जिसका अंत मगध सम्राट महापद्मनंद द्वारा किया गया।
विरोचन के पश्चात् दैत्यपति के पद पर समुद्र-मंथन का नायक रहा, उसका पराक्रमी पुत्र बलि आरूढ़ हुआ। सिंहासनारूढ़ होने के तुरंत पश्चात् पिता की हार का बदला लेते हुए उसने तात्कालिक इंद्र के महिमामयी पद पर अधिष्ठित होकर इस प्रतापी दैत्य ने सातों पातालों समेत पश्चिमी एशिया व यूरोप के सभी राजवंशों को जीतकर ‘त्रिलोकी’ के नाम से विख्यात हुआ (बलिनाऽधिष्ठिते चैव पुरा लोकत्रयेक्रमात्-मस्त्य पुराण-47/36)। बलि एक कुशल योद्धा तथा सफल प्रकाशक होने के साथ-साथ मुक्त हस्त से दान करनेवाला एक उदार नृप भी रहा था। उसकी इस कमजोर नस को भाँपते हुए विष्णु ने देवहित में बलि को उद्यमजनित विजय को पराजय में बदलने के लिए छल का सहारा लिया। धर्मनिष्ठ बलि द्वारा आयोजित एक यज्ञ-अनुष्ठान में विष्णु द्वारा भेजे गए नाटे कद के ‘बटुक’ ने उससे यज्ञ कर्म के लिए तीन पग भूमि दान में माँगी। वामन रूपी उस याचक के इस छुद्र प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करते हुए बलि ने उसे इच्छित स्थान पर भूमि को नापकर अपने अधिकार में लेने की राजाज्ञा जारी कर दी। वामन की इस कूट माँग को देव-षड्यंत्र का एक हिस्सा मानते हुए गुरु शुक्राचार्य ने बलि को समझाना चाहा और अंत में उसके इस दैत्यघाती निर्णय से क्षुब्ध होकर वे शाकद्वीप (अरब) चले गए। यहीं पर शुक्राचार्य ने अपने आराध्य शिव के लिंग को स्थापित कर एक भव्य मंदिर बनवाया था, जो कालांतर में ‘काव्य का मंदिर’ व तदनुरूप ‘काबा’ के नाम से विख्यात हुआ।
इधर बलि के निर्देशानुसार ‘तीन पग भूमि’ के क्रम से अग्निकुंडों को स्थापित करते हुए वामन व उसके सहयोगी दैत्यों के नगरों तथा पुरों को अपने अधिकार में करते चले गए। बलि द्वारा पूछे जाने पर वामन रूपी उस याचक ने तीन पगों का आशय वेद वर्णित ब्रह्म के पदों से (पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादयाभृतं दिवि-ऋ.-10-90-3) करते हुए उसे निरूत्तर कर दिया। अपनी वचनबद्धता के कारण निरुपाय हो चुके बलि को अंततोगत्वा राजमहल तक का त्याग करते हुए बंधु-बांधवों सहित सातों पातालों में से एक रहे सुतल (बलख) के दुरूह क्षेत्र में जाकर आश्रय लेना पड़ा था (सुतलं नाम पातालं त्वमासाद्य मनोरमम् वसासुर ममाऽऽदेशं यथावत्परिपालयन्-मत्स्य पुराण-246/75)। इस प्रकार त्रिलोक विजयी बलि को अपने जीवन का अंतिम समय सुतल स्थित ‘बलसुरा’ (बलि असुर के प्रतीकात्मक नगर जिसको कालांतर में बलख के नाम से जाना जाने लगा) के कष्टमयी वातावरण में बिताना पड़ा था।
प्राकृतिक त्रासदियों के लंबे दौर के पश्चात् इसलाम के दूसरे खलीफा उमर द्वारा 640 ईस्वी में पुन: बसाए गए इस नगर को अब ‘बसरा’ के नाम से जाना जाता है। महाप्राण बलि के पराभव के पश्चात् देवों (पुरंदर आदि इंद्र) का उसके उत्तराधिकारियों से निरंतर सात युद्ध हुए, जो आडीवक, त्रिपूर, अंधक, वृत्रघातक, धात्र हलाहल व कोलाहल नामक ‘देवासुर संग्रामों’ के रूप में विख्यात हुए (संदर्भ-मत्स्य पुराण-47/44.45)। इन देवासुर संग्रामों के पश्चात् दैत्य शक्ति का संपूर्ण विनाश हो गया और देवताओं का वर्चस्व संपूर्ण धरती पर व्याप्त हो गया। हिरण्याक्ष व फिर हिरण्यकशिपु के वधों में सक्रिय भूमिका निभानेवाले वाराहों व नृप-सिंह-देव (नरसिंह देव) तथा पराक्रमी बलि को पदच्युत करानेवाले याचक वामन के कृत्यों के सूत्रधार चूँकि अदिति-पुत्र विष्णु (पौराणिक पुरुष) ही रहे थे, अत: कालांतर में अवतारवाद से प्रभावित ग्रंथों में वाराह, नरसिंह, बामन आदि को विष्णु के ही विभिन्न स्वरूपों के रूप में मान्यताएँ प्रदान करते हुए नाम एकरूपता के कारण इन्हें सृष्टिकर्ता (विष्णु) के अधिभौतिक स्वरूपों (हयग्रीव, कच्छप आदि) की कड़ी से जोड़ दिया गया।
देव-उत्कर्ष के इसी काल में घटित प्रलय की भयंकर त्रासदी के कारण इस क्षेत्र में धन-जन की व्यापक हानि हुई। इस प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप त्रिविष्टप क्षेत्र में रह रहे देवों के कुछ समूहों को छोड़कर पश्चिमी एशिया का उनका साम्राज्य एकदम से नष्टप्राय: हो गया। त्रिविष्टप के इन्हीं देवों में से एक युवक ने आदित्य-कुल के बचे हुए बुजुर्गों के परामर्शों की अनदेखी करते हुए स्वयं को इनका अधिपति घोषित कर दिया। अपने इस निर्णय का विरोध करने पर इस महत्वाकांक्षी देवराट् अद्भुत (इंद्र) ने अपने पिता द्यौस की भी हत्या कर दी थी (संदर्भ-ऋ.4/18)। देवराट् ‘अद्भुत’ नामक इस इंद्र ने त्रिविष्टप स्थित नए देवलोक के पड़ोसी गणों (यक्ष, नाग, गंधर्व आदि) को अपना मित्र बनाते हुए अपने राज्य की प्रतिरोधात्मक क्षमता को सुरक्षित करके देव-वर्चस्व को पुन: प्रतिष्ठापित किया।
देवराट् ‘अद्भुत’ के ही काल में विवस्वान (सूर्य) के पुत्र वैवस्वत मनु मत्स्यों (मछुआरों) के सक्रिय सहयोग से जलप्लावन की त्रासदी से बंधु-बांधवों सहित स्वयं को सुरक्षित बचाते हुए भारत के सिंधु प्रांत में आकर विस्थापित हुए थे। मनु के पलायन कर जाने के बाद उनके विमाता के पुत्र रहे यम ही पितरों के राज्य के स्वामी बने थे। मनु पुत्र इक्ष्वाकु ने भारत के हृदय स्थल (कोशल) में सूर्यवंश की नींव डाली। इसी सूर्यवंश में युवनाश्व, मांधाता, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, भगीरथ, दिलीप, सुदास, रघु, दशरथ, राम आदि प्रतापी सम्राट हुए। इक्ष्वाकु के इस कालजयी कुल का अंतिम शासक सुमित्र हुआ, जिसका वध शैशुनाग वंशी उदायिभद्र के द्वारा किया गया था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i