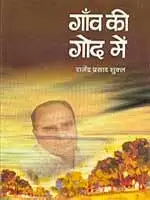|
जीवन कथाएँ >> गाँव की गोद में गाँव की गोद मेंराजेंन्द्र मोहन शुक्ल
|
282 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है गाँव की गोद में....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
जीवन प्रवाह में बहते हुए मैने गाँव की गोद में के माध्यम से ग्राम्य
संस्कृति के मुग्धकारी दृश्यों,रस्मो-रिवाज तीज-त्योहारों का और ऋतुओं का
जिक्र किया है,क्योंकि गाँव से ही मैने साहित्य पूजन और लोक सेवा का कार्य
आरंभ किया था। उस समय राजनीति में आने की संभावना तो क्या,अनुमान भी नहीं
था। साहित्य सृजन से भी कुछ यश मिल सकता है,इसका भी मुझे अंदाज नहीं था।
आगे चलकर मेरे रचनात्मक कार्यों से भी मुझे रचनाधर्मिता से जुड़े रहने के
प्रति प्रेरित किया।
सनद रहे
अवकाश के क्षणों में आपबीती को मैंने कलमबद्ध
कर लिया था। लिखने
के दौरान
यह भान नहीं था कि कभी यह पुस्तक का स्वरूप ग्रहण कर लेगा। इष्ट मित्रों
और परिवारजनों का विशेष आग्रह था कि जीवन की ऊँची-नीची, रपटीली राहों पर
चलकर जो उपलब्धियाँ और संघर्षों की कही-अनकही बातें थीं, जो यादगार प्रसंग
हैं, कैसे विषम परिस्थितियों से जूझते हुए जीवन-पथ पर चलता रहा, वह सुधी
समाज के बीच भी प्रकट हो।
आशा-निराशा के झंझावातों के घात-प्रतिघातों से वांछित प्राप्य समीप आकर भी दूर हो जाता है। छुटपन की कौतूहल तथा यौवन की रंगीन कल्पना प्रौढ़ता में यथार्थ के धरातल पर वास्तविक आकार-प्रकार ग्रहण कर लेती है। द्वंद्वात्मक सृष्टि में आशा-निराशा के बीच प्रबल प्रत्याशा की पिपासा संघर्ष के लिए उत्प्रेरित करती है। भावनाओं को शब्दों का जामा पहनाने का मेरा स्वभाव विद्यार्थी जीवन से ही रहा है। ग्राम्य जीवन की बाँकी झाँकी ने जहाँ मुझमें काव्यानुराग का संचरण किया वहीं सामाजिक कार्यों, खादी-प्रसार, ग्राम्य-स्वराज अभियान, सहकारिता के क्रियाकलापों और भू-आंदोलन की सहभागिता ने उन प्रसंगों को लिपिबद्ध करने के लिए प्रेरित किया, जिनका मेरे निर्माण में व्यापक योगदान है। परिस्थितिजन्य तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक घटनाक्रम के साथ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए मैंने अपने जीवन की घटनाओं को कालक्रम से प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास किया है।
दैनिक जीवन में घटित घटनाओं के साथ अपनी भावनाओं और क्रियाकलापों को संबद्ध कर लें तो वह आत्मकथा का स्वरूप ग्रहण कर लेता है और उससे प्राप्त अनुभव मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद भी हो सकते हैं। जीवन प्रवाह में बहते हुए मैंने ‘गाँव की गोद में’ के इस प्रथम खंड में ग्राम्य संस्कृति के मुग्धकारी दृश्यों, रस्मो-रिवाज, तीज-त्योहारों का और ऋतुओं का जिक्र किया है; क्योंकि गाँव से ही मैंने साहित्य-सृजन और लोक-सेवा का कार्य आरंभ किया था। उस समय राजनीति में आने की संभावना तो क्या, अनुमान भी नहीं था। साहित्य-सृजन से कुछ यश मिल सकता है, इसका भी मुझे अंदाज नहीं था। आगे चलकर मेरे रचनात्मक कार्यों ने भी मुझे रचनाधर्मिता से जुड़े रहने के प्रति प्रेरित किया।
मैंने अपनी आपबीती को आकार देने की हिमाकत तो कर ही दी है, मूल्यांकन का दायित्व नीर-क्षीर विवेकी पाठकों पर है।
इस कृति को आकार देने में डॉं. राजन यादव के सहयोग के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।
आशा-निराशा के झंझावातों के घात-प्रतिघातों से वांछित प्राप्य समीप आकर भी दूर हो जाता है। छुटपन की कौतूहल तथा यौवन की रंगीन कल्पना प्रौढ़ता में यथार्थ के धरातल पर वास्तविक आकार-प्रकार ग्रहण कर लेती है। द्वंद्वात्मक सृष्टि में आशा-निराशा के बीच प्रबल प्रत्याशा की पिपासा संघर्ष के लिए उत्प्रेरित करती है। भावनाओं को शब्दों का जामा पहनाने का मेरा स्वभाव विद्यार्थी जीवन से ही रहा है। ग्राम्य जीवन की बाँकी झाँकी ने जहाँ मुझमें काव्यानुराग का संचरण किया वहीं सामाजिक कार्यों, खादी-प्रसार, ग्राम्य-स्वराज अभियान, सहकारिता के क्रियाकलापों और भू-आंदोलन की सहभागिता ने उन प्रसंगों को लिपिबद्ध करने के लिए प्रेरित किया, जिनका मेरे निर्माण में व्यापक योगदान है। परिस्थितिजन्य तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक घटनाक्रम के साथ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए मैंने अपने जीवन की घटनाओं को कालक्रम से प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास किया है।
दैनिक जीवन में घटित घटनाओं के साथ अपनी भावनाओं और क्रियाकलापों को संबद्ध कर लें तो वह आत्मकथा का स्वरूप ग्रहण कर लेता है और उससे प्राप्त अनुभव मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद भी हो सकते हैं। जीवन प्रवाह में बहते हुए मैंने ‘गाँव की गोद में’ के इस प्रथम खंड में ग्राम्य संस्कृति के मुग्धकारी दृश्यों, रस्मो-रिवाज, तीज-त्योहारों का और ऋतुओं का जिक्र किया है; क्योंकि गाँव से ही मैंने साहित्य-सृजन और लोक-सेवा का कार्य आरंभ किया था। उस समय राजनीति में आने की संभावना तो क्या, अनुमान भी नहीं था। साहित्य-सृजन से कुछ यश मिल सकता है, इसका भी मुझे अंदाज नहीं था। आगे चलकर मेरे रचनात्मक कार्यों ने भी मुझे रचनाधर्मिता से जुड़े रहने के प्रति प्रेरित किया।
मैंने अपनी आपबीती को आकार देने की हिमाकत तो कर ही दी है, मूल्यांकन का दायित्व नीर-क्षीर विवेकी पाठकों पर है।
इस कृति को आकार देने में डॉं. राजन यादव के सहयोग के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।
एक
मैं मूलतः गाँव का व्यक्ति हूँ। मेरा ननिहाल
बिलासपुर में है। मेरा जन्म
10 फरवरी, 1930 को बिलासपुर में हु्आ; लेकिन मेरा लालन-पालन, प्रथमिक
शिक्षा पूर्णरूपेण बिलासपुर से पैंसठ कि.मी. दूर एक देहात में, जिसे
सिंघनपुरी बाजार कहा जाता है, वहीं हुई। उस समय बिलासपुर की सड़कों पर तो
क्या, घरों में भी बिजली नहीं थी। मुझे याद है, जब मैं अपने नाना-नानी के
घर बिलासपुर आया करता था तो रात में वहाँ ढिबरी जलाई जाती थी। लालटेन बाहर
और भीतर जलाई जाती थी। बिलासपुर की सड़कों पर उस समय नगरपालिका के लैंप
पोस्ट में मिट्टी के तेल के चिराग म्यूनिसिपल काउंसिल के चपरासी शाम को
जगह-जगह जलाते थे। बिलासपुर के गोल बाजार में हमारे मामाजी का घर है। वहाँ
अकसर हम लोग ठहरा करते थे। उनके पास ही म्यूनिसिपल स्कूल है। पहले वहाँ
केवल अठवीं कक्षा तक पढ़ाई होती थी। यह बिलासपुर जिले में एकमात्र
गवर्नमेंट हाई स्कूल था, जो मुख्य मार्ग पर जूना बिलासपुर के बाद, दयालबंद
मोहल्ले की शुरुआत में स्थित था। म्यूनिसिपल काउंसिल का एक चपरासी, जो
काफी वृद्ध था, रंगीन छींट की पूरी बाँही कमीज के ऊपर काली फतोही पहन, सिर
पर एक अँगोछा लपेटकर, कंधे पर सीढ़ी रखे शाम होने के पहले धुँधलके में ही
जगह-जगह लैंप पोस्ट के चिरागों के जलाया करता था। हम कौतूहल से उसे देखते
थे। बिलासपुर शहर की मुख्य सड़क भी डामर की नहीं, गिट्टी और मुरुम की ही
थी। बहुत सी गलियों की सड़कें तो साधराण और कच्ची ही थीं। शहर की जनसंख्या
उस समय बीस-पच्चीस हजार की ही रही होगी। देहातों की हालत तो बहुत ही खराब
थी। तखतपुर कोटा और लोरमी आज जिस स्थिति में हैं, कल्पना नहीं की जा सकती
कि उस समय कितनी बुरी हालत रही होगी। बिलासपुर से तखतपुर होते हुए मूँगेली
के लिए अमर ट्रांसपोर्ट और विजय ट्रांसपोर्ट की केवल एक बस सबेरे-शाम चलती
थी। आजकल उन्हीं सड़कों पर सैकड़ों बसें, टैंपो, टैक्सी, ट्रक आदि वाहन
चला करते हैं। बिलासपुर से तखतपुर भी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं था।
बीच में दो नाले थे, जिन पर पुल नहीं बना था। थोड़ी सी बरसात हो जाने पर
यातायात रुक जाता था। यही किस्सा तखतपुर से मुँगेली का था। उनमें से कुछ
सड़कें कुछ दूर तक गिट्टी और मुरुम की तथा कच्ची थीं। कच्ची सड़कों पर
बरसात में गाड़ी फँस जाया करती थी, इसलिए निश्चित नहीं था कि बस चलेगी ही।
बिलासपुर से कोटा की सड़क तो और भी खराब थी।
दूसरे महायुद्ध सन् 1944-45 के समय कोटा की सड़क गिट्टी और मुरुमवाली बनाई गई। उसी समय कोटा के आगे आठ-नौ कि.मी. तक गिट्टीवाली सड़क बनाई गई। इन सड़कों पर भी पुल-पुलियों का अभाव था। कोटा से आगे छोटी करगी के बाद लोरमी और पंडरिया तक का रास्ता धूल और कीचड़ का था। सूखे के दिनों में मिट्टी और मुरुम का चूर्ण बनकर करीब दो-तीन फिट धूल हो जाती थी। पहले तो इस लाइन पर एक भी बस नहीं चलती थी; लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद या यों कहें कि सन्’ 47 के बाद गरमियों में ही कोटा के आगे बस जाती थी। कोटा तक येन-केन-प्रकारेण यदा-कदा एक दो बसें दिन में चल जाती थीं। तखतपुर बिलासपुर से अठारह मील यानी इकतीस कि.मी. की दूरी पर है और तखतपुर के आगे हम लोगों का गाँव बाजार सिंघनपुरी बारह मील यानी अठारह कि.मी. के फासले पर है। उसी प्रकार कोटा के रास्ते जाने पर छोटी करगी के बाद लगभग बीस-बाइस कि.मी. चलने पर हम लोगों का गाँव जूनापारा है, जहाँ अब हम पारिवारिक बँटवारे के बाद अलग से स्थायी रूप से रहने लगे हैं। यह रास्ता जैसाकि मैं कह चुका हूँ, कच्चा ही था। ऐसा बताया जाता है कि सन् 1890 और ’98 के बीच अकाल पड़ने पर करगी और पंडरिया के जमीदारों ने अंग्रेज सरकार के समय कच्ची सड़कें बनवाई थीं। किनारे-किनारे बड़े-बड़े वृक्ष थे, जिनकी सघन छाया रहती थी।
जूनापारा पहुँचने के बाद वहाँ से तीन कि.मी. सीधी पगडंडी के रास्ते में घुटने तक, बल्कि जाँघ के ऊपर तक काली मिट्टी का दलदल हो जाया करता था। बैलगाड़ी से या पैदल चलना भी मुश्किल काम था। चारों तरफ घने जंगल थे। गाँव भी एक प्रकार से जंगलों के बीच में ही था। जंगली जानवर भी गाँव के आस-पास आ जाया करते थे। मैंने बचपन में तथा अपने शिक्षा काल में कई बार बाजार सिंघनपुरी के नाले के पास जानवरों के आने की घटनाएँ सुनी थीं। ये जंगली जानवर गाहे-बगाहे आदमियों को तो नहीं, लेकिन घरेलू पशुओं का जरूर घात लगाकर शिकार किया करते थे। हमारे गाँव बाजार सिंघनपुरी के पास से नीचे मनियारी नदी बहती है। उत्तर में पाँच-छह कि.मी. के बाद मेकल की पर्वत श्रेणियाँ हैं। पश्चिम की ओर एक फुलवारी नाम का नाला बहता है। मनियारी नदी में नवंबर-दिसंबर तक तो बहता हुआ पानी रहता है, उसके बाद कहीं-कहीं थोड़ा, तो कुछ जगह गहराई में ज्यादा पानी रहता है। गाँव में रास्ते और सड़क होने का सवाल ही नहीं उठता। बिजली की रोशनी बिलासपुर में नहीं थी, तो गाँव में होने का प्रश्न ही नहीं था। बाजार सिंघनपुरी में प्रथमिक शाला भी नहीं थी। वहाँ से हम लोग तीन कि.मी. पैदल चलकर रानी डेरा नामक गाँव में पढ़ने जाते थे। प्रथमिक शाला की पढ़ाई उस समय चार दरजे तक होती थी। चौथी के बाद मिडिल स्कूल में प्रवेश लेना होता था। पाँच साल की उम्र से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। उस समय गाँव के स्कूलों में पढ़ाई सुबह और शाम, दो अलग-अलग पारियों में होती थी, इसलिए सुबह जल्दी तैयार होकर रानीडेरा जाते थे। वहाँ से बारह बजे दोपहर छुट्टी होने पर पैदल बाजार सिंघनपुरी आते थे।
सुबह आमतौर पर खिचड़ी और अचार का नाश्ता होता था। खिचड़ी चावल और मूँग या अरहर की दाल को मिलाकर पकाई जाती थी। साथ में आम या नीबू का अचार या कोई चटनी होती थी। बारह बजे स्कूल से लौटने के बाद थककर चूर हो जाते थे। मुँह धूप में लाल हो जाता था। आने के बाद हमारे लिए अलग से छोटे-छोटे गिलास, जिसको घंटी कहते हैं, में एक-एक घंटी दूध-जो करीब सौ या अधिक-से-अधिक डेढ़ सौ मिली लीटर रहता रहा होगा-रखा रहता था। उसको पीने के बाद मनियारी नदी में तैरने जाते थे वहाँ जाकर घंटों पानी में छपकियाँ लगाते थे। पहले तो जब छोटे थे तब गहरे पानी में जाने से भय लगता था। किनारे बैठे रहते थे। कोई लड़का अगर शैतानी करके ढकेल देता था तो डुबकी लगाते हुए उभुक-चुभुक करने लगते थे। फिर कोई पकड़कर बाहर करता था। उस समय पिताजी हम लोगों को ढूँढ़ते हुए आते थे और मार भी पड़ती थी। अधिकतर समय नदी में रेत पर सीपियाँ ढूँढ़ने, इकट्ठा करने और रेत के घर बनाने में बीत जाता था। फिर पिताजी की जोरों से डाँट पड़ती थी। उनकी रोबीली आवाज सुनाई पड़ती थी तो दौड़कर पीछे के दरवाजे से भागकर माँ के पास छिप जाते थे। खाना खाने के बाद फौरन मुँह पोछते, बस्ता टाँगते, फिर शाम के स्कूल हेतु रानीडेरा जाते थे।
उस समय गाँव के अन्य लड़के भी हमारे साथ स्कूल जाते थे। हम लोग गाँव के मालगुजार थे। हमारे पूर्वजों के पास बाजार सिंघनपुरी के अलावा जूनापारा, कठमुंडा, रैयतवारी कंचनपुर, बरगन, ठरगपुर, पैजनिया आदि गाँव थे। अपने परिवार की कहानी अलग से लिखूँगा। मैं अभी उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। कुछ समय के लिए हमारे पिताजी ने दो छोटे-छोटे पट्टू लिये थे। मेरे साथ सगे चचेरे भाई, जो मुझसे उम्र में नौ दिन बड़े हैं, शारदा प्रसाद शुक्ल, बाजार सिंघनपुरी में रहकर खेती का काम देखते हैं, वे भी जाते थे। वे अभी भी वहीं रहते हैं। हालाकि उन्होंने बिलासपुर में मकान-जायदाद बना लिया है।
उनके लड़के भी सब काम में लग गए हैं। हमारे साथ देख-रेख करनेवाले एक टीकाराम पंडितजी थे। उनका वर्णन करना जरूरी है। उनकी लंबी चुटिया किसी रेडियो के एरियल के समान खड़ी रहती थी। उनके बाल आधे इंच से भी कम रहते थे। हाफ कमीज और घुटनों तक गमछानुमा धोती, चमरौंधा जूता और उनके हाथ में एक पतली छड़ी रहती थी। उनके माथे पर चंदन का टीका अवश्य रहता था। वे हमारे साथ जाते थे। सिंघनपुरी में हमारे घर के सामने आठ-दस बड़े मंदिर हैं। उतनी ऊँचाई के मंदिर मैंने बिलासपुर में भी नहीं देखे थे। हमारे प्रपितामह, जो पहली बार मिदनापुर या उन्नाव जिले से मिदनापुर होते हुए बिलासपुर आए थे, ने उन मंदिरों को बनवाया था। उन मंदिरों में पहले हरदेव लाल पंडित पूजा करते थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद श्री टीकारामजी पूजा करने लगे। श्री टीकारामजी जीवन-पर्यंत हमारे परिवार से जुड़े रहे। हमारे चौथी पास करने तक उनका काम हमें स्कूल छोड़ना, साथ में रहना और फिर वापस लाना था। वे अकेले और अविवाहित थे। उनको अफीम का मदक बनाकर पीने की आदत थी। कभी-कभी गाँजे का कस लगाते हुए भी देखा था, अकसर वह बीड़ी पीते थे। मदक बनाकर पीने की वजह से सामान्य तौर पर लोग-बाग उनको ‘मदक्की-मदक्की’ कहकर बुलाते और चिढ़ाते थे। टीकारामजी हमारे साथ बातचीत में बड़े अच्छे थे। ढेरों कहानी-किस्से सुनाते थे। कुछ नहीं तो रास्ते में कुछ-न-कुछ गुनगुनाते और गाते हुए चलते थे। मुझे याद है, बीमार पड़ने पर वे अकसर गाया करते थे-
दूसरे महायुद्ध सन् 1944-45 के समय कोटा की सड़क गिट्टी और मुरुमवाली बनाई गई। उसी समय कोटा के आगे आठ-नौ कि.मी. तक गिट्टीवाली सड़क बनाई गई। इन सड़कों पर भी पुल-पुलियों का अभाव था। कोटा से आगे छोटी करगी के बाद लोरमी और पंडरिया तक का रास्ता धूल और कीचड़ का था। सूखे के दिनों में मिट्टी और मुरुम का चूर्ण बनकर करीब दो-तीन फिट धूल हो जाती थी। पहले तो इस लाइन पर एक भी बस नहीं चलती थी; लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद या यों कहें कि सन्’ 47 के बाद गरमियों में ही कोटा के आगे बस जाती थी। कोटा तक येन-केन-प्रकारेण यदा-कदा एक दो बसें दिन में चल जाती थीं। तखतपुर बिलासपुर से अठारह मील यानी इकतीस कि.मी. की दूरी पर है और तखतपुर के आगे हम लोगों का गाँव बाजार सिंघनपुरी बारह मील यानी अठारह कि.मी. के फासले पर है। उसी प्रकार कोटा के रास्ते जाने पर छोटी करगी के बाद लगभग बीस-बाइस कि.मी. चलने पर हम लोगों का गाँव जूनापारा है, जहाँ अब हम पारिवारिक बँटवारे के बाद अलग से स्थायी रूप से रहने लगे हैं। यह रास्ता जैसाकि मैं कह चुका हूँ, कच्चा ही था। ऐसा बताया जाता है कि सन् 1890 और ’98 के बीच अकाल पड़ने पर करगी और पंडरिया के जमीदारों ने अंग्रेज सरकार के समय कच्ची सड़कें बनवाई थीं। किनारे-किनारे बड़े-बड़े वृक्ष थे, जिनकी सघन छाया रहती थी।
जूनापारा पहुँचने के बाद वहाँ से तीन कि.मी. सीधी पगडंडी के रास्ते में घुटने तक, बल्कि जाँघ के ऊपर तक काली मिट्टी का दलदल हो जाया करता था। बैलगाड़ी से या पैदल चलना भी मुश्किल काम था। चारों तरफ घने जंगल थे। गाँव भी एक प्रकार से जंगलों के बीच में ही था। जंगली जानवर भी गाँव के आस-पास आ जाया करते थे। मैंने बचपन में तथा अपने शिक्षा काल में कई बार बाजार सिंघनपुरी के नाले के पास जानवरों के आने की घटनाएँ सुनी थीं। ये जंगली जानवर गाहे-बगाहे आदमियों को तो नहीं, लेकिन घरेलू पशुओं का जरूर घात लगाकर शिकार किया करते थे। हमारे गाँव बाजार सिंघनपुरी के पास से नीचे मनियारी नदी बहती है। उत्तर में पाँच-छह कि.मी. के बाद मेकल की पर्वत श्रेणियाँ हैं। पश्चिम की ओर एक फुलवारी नाम का नाला बहता है। मनियारी नदी में नवंबर-दिसंबर तक तो बहता हुआ पानी रहता है, उसके बाद कहीं-कहीं थोड़ा, तो कुछ जगह गहराई में ज्यादा पानी रहता है। गाँव में रास्ते और सड़क होने का सवाल ही नहीं उठता। बिजली की रोशनी बिलासपुर में नहीं थी, तो गाँव में होने का प्रश्न ही नहीं था। बाजार सिंघनपुरी में प्रथमिक शाला भी नहीं थी। वहाँ से हम लोग तीन कि.मी. पैदल चलकर रानी डेरा नामक गाँव में पढ़ने जाते थे। प्रथमिक शाला की पढ़ाई उस समय चार दरजे तक होती थी। चौथी के बाद मिडिल स्कूल में प्रवेश लेना होता था। पाँच साल की उम्र से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। उस समय गाँव के स्कूलों में पढ़ाई सुबह और शाम, दो अलग-अलग पारियों में होती थी, इसलिए सुबह जल्दी तैयार होकर रानीडेरा जाते थे। वहाँ से बारह बजे दोपहर छुट्टी होने पर पैदल बाजार सिंघनपुरी आते थे।
सुबह आमतौर पर खिचड़ी और अचार का नाश्ता होता था। खिचड़ी चावल और मूँग या अरहर की दाल को मिलाकर पकाई जाती थी। साथ में आम या नीबू का अचार या कोई चटनी होती थी। बारह बजे स्कूल से लौटने के बाद थककर चूर हो जाते थे। मुँह धूप में लाल हो जाता था। आने के बाद हमारे लिए अलग से छोटे-छोटे गिलास, जिसको घंटी कहते हैं, में एक-एक घंटी दूध-जो करीब सौ या अधिक-से-अधिक डेढ़ सौ मिली लीटर रहता रहा होगा-रखा रहता था। उसको पीने के बाद मनियारी नदी में तैरने जाते थे वहाँ जाकर घंटों पानी में छपकियाँ लगाते थे। पहले तो जब छोटे थे तब गहरे पानी में जाने से भय लगता था। किनारे बैठे रहते थे। कोई लड़का अगर शैतानी करके ढकेल देता था तो डुबकी लगाते हुए उभुक-चुभुक करने लगते थे। फिर कोई पकड़कर बाहर करता था। उस समय पिताजी हम लोगों को ढूँढ़ते हुए आते थे और मार भी पड़ती थी। अधिकतर समय नदी में रेत पर सीपियाँ ढूँढ़ने, इकट्ठा करने और रेत के घर बनाने में बीत जाता था। फिर पिताजी की जोरों से डाँट पड़ती थी। उनकी रोबीली आवाज सुनाई पड़ती थी तो दौड़कर पीछे के दरवाजे से भागकर माँ के पास छिप जाते थे। खाना खाने के बाद फौरन मुँह पोछते, बस्ता टाँगते, फिर शाम के स्कूल हेतु रानीडेरा जाते थे।
उस समय गाँव के अन्य लड़के भी हमारे साथ स्कूल जाते थे। हम लोग गाँव के मालगुजार थे। हमारे पूर्वजों के पास बाजार सिंघनपुरी के अलावा जूनापारा, कठमुंडा, रैयतवारी कंचनपुर, बरगन, ठरगपुर, पैजनिया आदि गाँव थे। अपने परिवार की कहानी अलग से लिखूँगा। मैं अभी उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। कुछ समय के लिए हमारे पिताजी ने दो छोटे-छोटे पट्टू लिये थे। मेरे साथ सगे चचेरे भाई, जो मुझसे उम्र में नौ दिन बड़े हैं, शारदा प्रसाद शुक्ल, बाजार सिंघनपुरी में रहकर खेती का काम देखते हैं, वे भी जाते थे। वे अभी भी वहीं रहते हैं। हालाकि उन्होंने बिलासपुर में मकान-जायदाद बना लिया है।
उनके लड़के भी सब काम में लग गए हैं। हमारे साथ देख-रेख करनेवाले एक टीकाराम पंडितजी थे। उनका वर्णन करना जरूरी है। उनकी लंबी चुटिया किसी रेडियो के एरियल के समान खड़ी रहती थी। उनके बाल आधे इंच से भी कम रहते थे। हाफ कमीज और घुटनों तक गमछानुमा धोती, चमरौंधा जूता और उनके हाथ में एक पतली छड़ी रहती थी। उनके माथे पर चंदन का टीका अवश्य रहता था। वे हमारे साथ जाते थे। सिंघनपुरी में हमारे घर के सामने आठ-दस बड़े मंदिर हैं। उतनी ऊँचाई के मंदिर मैंने बिलासपुर में भी नहीं देखे थे। हमारे प्रपितामह, जो पहली बार मिदनापुर या उन्नाव जिले से मिदनापुर होते हुए बिलासपुर आए थे, ने उन मंदिरों को बनवाया था। उन मंदिरों में पहले हरदेव लाल पंडित पूजा करते थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद श्री टीकारामजी पूजा करने लगे। श्री टीकारामजी जीवन-पर्यंत हमारे परिवार से जुड़े रहे। हमारे चौथी पास करने तक उनका काम हमें स्कूल छोड़ना, साथ में रहना और फिर वापस लाना था। वे अकेले और अविवाहित थे। उनको अफीम का मदक बनाकर पीने की आदत थी। कभी-कभी गाँजे का कस लगाते हुए भी देखा था, अकसर वह बीड़ी पीते थे। मदक बनाकर पीने की वजह से सामान्य तौर पर लोग-बाग उनको ‘मदक्की-मदक्की’ कहकर बुलाते और चिढ़ाते थे। टीकारामजी हमारे साथ बातचीत में बड़े अच्छे थे। ढेरों कहानी-किस्से सुनाते थे। कुछ नहीं तो रास्ते में कुछ-न-कुछ गुनगुनाते और गाते हुए चलते थे। मुझे याद है, बीमार पड़ने पर वे अकसर गाया करते थे-
अब न बचे बचाए ले चोला,
अब न बचे बचाय ले राम !
अब न बचे बचाय ले राम !
यह गाना छत्तीसगढ़ी में हुआ करता था। हम लोग
भी आपस में छत्तीसगढ़ी में ही
बात करते थे। चौथी पास करने के बाद बिलासपुर गए तो हमें हिंदी बोलने में
कठिनाई होती थी। बिलासपुर में शहर के लड़के हमें देहाती या छत्तीसगढ़िया
कहते थे, जिसका उस समय हम आशय नहीं समझ पाते थे।
बिलासपुर के मिडिल स्कूल में भरती होने के बाद भी हम आठवीं-नौवीं कक्षा तक बिना जूते-चप्पल के ही रहे। जूते केवल दशहरा में ही खरीदे जाते थे। उन्हें खास अवसरों पर ही पहना करते थे। पं. टीकारामजी के साथ टट्टू पर बैठकर जाने का भी हमने आनंद लिया। जब हम पाँच या छह साल के थे, टट्टू पर बैठना नहीं आता था। धीरे-धीरे आदत पड़ी। रानीडेरा, खेतों की मेड़ों पर से जाया जाता था। बीच-बीच में खोतों की मेड़ टूटी रहती थी, जिसमें से एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता था। बरसात में लबालब पानी हो जाया करता था, बहता भी था। ये टट्टू फूटे हुए मुहियों को लाँघने के लिए कूदते थे, उस कूदने को ‘चौपी कूदना’ कहा जाता है। जैसे ही वे चौपी कूदते थे, मैं और मेरे चचेरे भाई पानी भरे खेत में गिर पड़ते थे। रोना मच जाता था। फिर टीकाराम पंडित हम लोगों को निकालते थे, पुचकारते थे, डाँटते थे। अगर कभी साथ में कपड़े रहे तो उन्हें बदलवाते थे, नहीं तो फिर नंगे बदन स्कूल जाना होता था। वहाँ पहुँचने के बाद कपड़े सुखाकर पहन लेते थे। बाद में मैंने रानीडेरा के नए स्कूल और मिडिल स्कूल का उद्घाटन भी किया। विधानसभा के अध्यक्ष की हैसियत से वहाँ मिडिल स्कूल भी मंजूर किया। दोनों समारोह वहाँ पर संपन्न हुए। पुराना स्कूल तालाब के पास था। मास्टर साहब अक्सर मिट्टी के मटके में हमसे तालाब से पानी भरवाते, पूरे स्कूल की झाड़ू लगवाते और लिपवाते थे। स्कूल के बाहर जो पौधे लगे रहते थे, उनमें पानी डालने का काम भी कराया जाता। हालाँकि हम ज्यादा मार नहीं खाए, लेकिन गुरूजी के कहने मात्र से भय मालूम पड़ता था। ऐसा मैंने देखा है कि छोटे बच्चे माता-पिता का कहना उतना नहीं मानते, जितना कि अपने गुरूजी का निर्देश मानते हैं। अगर गुरूजी के निर्देशानुसार कार्य पूरा न हो तो रो-रोकर घर सिर पर उठा लेते हैं।
सिंघनपुरी और रानीडेरा के बीचोबीच एक और तालाब पड़ता था, जिसे ‘मद्धू तालाब’ कहते हैं। कुछ इस प्रकार की किंवदंती थी कि मद्धू तालाब में भूत रहते हैं, बड़े-बड़े मगर रहते हैं, जो जंजीर बन गए हैं। किसी भी आदमी को पकड़कर खा लेते हैं, कँसकर मार डालते हैं। उस तालाब की मेड़ के ऊपर से चलकर रानीडेरा पहुँचना होता था। तालाब के ऊपर पहुँचते ही हम राम-राम जपना या हनुमानजी को याद करना शुरू कर देते थे। मेरा ऐसा खयाल है कि यह जगह सुनसान है, दो गाँवों के बीच की दूरियों पर है। इसलिए शायद इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई होगी। रानीडेरा के स्कूल में मुझे जिन प्रारंभिक शिक्षक का स्मरण आता है उनका नाम चेतनदास था। वे गंजे सिर, गठे शरीर, साँवले बदन के सीदे-सादे व्यक्ति थे। वहाँ एक मुसलमान गुरूजी ईदू मियाँ भी थे। तखतपुरवाले कादर मियाँ उनके चोटे भाई थे, जिनके लड़के अभी भी साधो-माधो के नाम से हैं। गुरूजी के बड़े भाई का नाम शेख था। बाजार सिंघनपुरी में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मोहल्ला है। मसजिद भी है। वहाँ ताजिया भी बनाते हैं। उनके रिश्तेदार वहाँ थे, इसलिए वे मुसलमान गुरूजी सिंघनपुरी में ही रहते थे। हम लोगों के साथ स्कूल आया-जाया करते थे। ये दोनों गुरूजी बड़े कड़े थे। विशेष रूप से कनबुच्ची लगवाने या मुरगा बनने का दंड देते थे। हम लोगों के साथ थोड़ी सी रहम की भावना रखते थे संभवतः इसलिए कि हम बड़े मालगुजार की संतान थे। उस स्कूल की जो कमेटी थी उसके सरपंच भी हमारे पिताजी थे। जब मैं चौथी में पढ़ रहा था उसके एकाध साल पहले से ग्राम पूरा, जो तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में है, के रहनेवाले गुरूजी कीर्तिराम साहू प्रधान पाठक थे। वे बहुत सज्जन थे। एम.एल.ए. और संसदीय सचिव बनने के बाद मैं ग्राम पूरा हो गया और उनको अपना प्रणाम भी निवेदित किया था। उनके साथ में नायब शिक्षक श्री केजाराम मास्टर साहब थे, जो जाति से कलार थे। वे लोरमी के पास डोंगरिया गाँव के रहनेवाले थे। केजारामजी भी सिंघनपुरी में रहते थे। हमारे घर के सामने एक मंदिर था, वहाँ पर जो बगीचा था उसमें एक छोटी परछी सरीखे थी, जिसमें कमरा और बरामदा था। वहीं हम लोगों को स्कूल के बाद पढ़ाते थे। उस समय मास्टरों की तनख्वाह बारह रुपये महीने थी। इतना जरूर था कि केजाराम गुरूजी को हमारे घर से सीधा यानी चावल और दाल आदि प्रतिदिन दे दिया जाता था। वे गाँव की गुड़ी में रहते थे। गुड़ी वह स्थान है, जो सार्वजनिक होता है। उसे गाँव का रेस्ट हाउस कहा जा सकता है। चौथी हिंदी पास होने तक कीर्तिरामजी और केजारामजी दोनों हमारे शिक्षक थे।
मैं छुटपन में बहुत दुबला-पतला था। आज के आकार-प्रकार को देखकर कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि मैं कभी उस प्रकार का दुबला-पतला रहा होऊँगा। उस, समय जब मोटे आदमियों को, स्वस्थ व्यक्तियों को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा हो पाऊँगा या नहीं। अब मुझे अपनी इस शारीरिक स्थिति पर स्वयं कई बार क्षोभ होता है। खैर, यह सब अपने हाथ में नहीं है।
बिलासपुर के मिडिल स्कूल में भरती होने के बाद भी हम आठवीं-नौवीं कक्षा तक बिना जूते-चप्पल के ही रहे। जूते केवल दशहरा में ही खरीदे जाते थे। उन्हें खास अवसरों पर ही पहना करते थे। पं. टीकारामजी के साथ टट्टू पर बैठकर जाने का भी हमने आनंद लिया। जब हम पाँच या छह साल के थे, टट्टू पर बैठना नहीं आता था। धीरे-धीरे आदत पड़ी। रानीडेरा, खेतों की मेड़ों पर से जाया जाता था। बीच-बीच में खोतों की मेड़ टूटी रहती थी, जिसमें से एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता था। बरसात में लबालब पानी हो जाया करता था, बहता भी था। ये टट्टू फूटे हुए मुहियों को लाँघने के लिए कूदते थे, उस कूदने को ‘चौपी कूदना’ कहा जाता है। जैसे ही वे चौपी कूदते थे, मैं और मेरे चचेरे भाई पानी भरे खेत में गिर पड़ते थे। रोना मच जाता था। फिर टीकाराम पंडित हम लोगों को निकालते थे, पुचकारते थे, डाँटते थे। अगर कभी साथ में कपड़े रहे तो उन्हें बदलवाते थे, नहीं तो फिर नंगे बदन स्कूल जाना होता था। वहाँ पहुँचने के बाद कपड़े सुखाकर पहन लेते थे। बाद में मैंने रानीडेरा के नए स्कूल और मिडिल स्कूल का उद्घाटन भी किया। विधानसभा के अध्यक्ष की हैसियत से वहाँ मिडिल स्कूल भी मंजूर किया। दोनों समारोह वहाँ पर संपन्न हुए। पुराना स्कूल तालाब के पास था। मास्टर साहब अक्सर मिट्टी के मटके में हमसे तालाब से पानी भरवाते, पूरे स्कूल की झाड़ू लगवाते और लिपवाते थे। स्कूल के बाहर जो पौधे लगे रहते थे, उनमें पानी डालने का काम भी कराया जाता। हालाँकि हम ज्यादा मार नहीं खाए, लेकिन गुरूजी के कहने मात्र से भय मालूम पड़ता था। ऐसा मैंने देखा है कि छोटे बच्चे माता-पिता का कहना उतना नहीं मानते, जितना कि अपने गुरूजी का निर्देश मानते हैं। अगर गुरूजी के निर्देशानुसार कार्य पूरा न हो तो रो-रोकर घर सिर पर उठा लेते हैं।
सिंघनपुरी और रानीडेरा के बीचोबीच एक और तालाब पड़ता था, जिसे ‘मद्धू तालाब’ कहते हैं। कुछ इस प्रकार की किंवदंती थी कि मद्धू तालाब में भूत रहते हैं, बड़े-बड़े मगर रहते हैं, जो जंजीर बन गए हैं। किसी भी आदमी को पकड़कर खा लेते हैं, कँसकर मार डालते हैं। उस तालाब की मेड़ के ऊपर से चलकर रानीडेरा पहुँचना होता था। तालाब के ऊपर पहुँचते ही हम राम-राम जपना या हनुमानजी को याद करना शुरू कर देते थे। मेरा ऐसा खयाल है कि यह जगह सुनसान है, दो गाँवों के बीच की दूरियों पर है। इसलिए शायद इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई होगी। रानीडेरा के स्कूल में मुझे जिन प्रारंभिक शिक्षक का स्मरण आता है उनका नाम चेतनदास था। वे गंजे सिर, गठे शरीर, साँवले बदन के सीदे-सादे व्यक्ति थे। वहाँ एक मुसलमान गुरूजी ईदू मियाँ भी थे। तखतपुरवाले कादर मियाँ उनके चोटे भाई थे, जिनके लड़के अभी भी साधो-माधो के नाम से हैं। गुरूजी के बड़े भाई का नाम शेख था। बाजार सिंघनपुरी में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मोहल्ला है। मसजिद भी है। वहाँ ताजिया भी बनाते हैं। उनके रिश्तेदार वहाँ थे, इसलिए वे मुसलमान गुरूजी सिंघनपुरी में ही रहते थे। हम लोगों के साथ स्कूल आया-जाया करते थे। ये दोनों गुरूजी बड़े कड़े थे। विशेष रूप से कनबुच्ची लगवाने या मुरगा बनने का दंड देते थे। हम लोगों के साथ थोड़ी सी रहम की भावना रखते थे संभवतः इसलिए कि हम बड़े मालगुजार की संतान थे। उस स्कूल की जो कमेटी थी उसके सरपंच भी हमारे पिताजी थे। जब मैं चौथी में पढ़ रहा था उसके एकाध साल पहले से ग्राम पूरा, जो तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में है, के रहनेवाले गुरूजी कीर्तिराम साहू प्रधान पाठक थे। वे बहुत सज्जन थे। एम.एल.ए. और संसदीय सचिव बनने के बाद मैं ग्राम पूरा हो गया और उनको अपना प्रणाम भी निवेदित किया था। उनके साथ में नायब शिक्षक श्री केजाराम मास्टर साहब थे, जो जाति से कलार थे। वे लोरमी के पास डोंगरिया गाँव के रहनेवाले थे। केजारामजी भी सिंघनपुरी में रहते थे। हमारे घर के सामने एक मंदिर था, वहाँ पर जो बगीचा था उसमें एक छोटी परछी सरीखे थी, जिसमें कमरा और बरामदा था। वहीं हम लोगों को स्कूल के बाद पढ़ाते थे। उस समय मास्टरों की तनख्वाह बारह रुपये महीने थी। इतना जरूर था कि केजाराम गुरूजी को हमारे घर से सीधा यानी चावल और दाल आदि प्रतिदिन दे दिया जाता था। वे गाँव की गुड़ी में रहते थे। गुड़ी वह स्थान है, जो सार्वजनिक होता है। उसे गाँव का रेस्ट हाउस कहा जा सकता है। चौथी हिंदी पास होने तक कीर्तिरामजी और केजारामजी दोनों हमारे शिक्षक थे।
मैं छुटपन में बहुत दुबला-पतला था। आज के आकार-प्रकार को देखकर कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि मैं कभी उस प्रकार का दुबला-पतला रहा होऊँगा। उस, समय जब मोटे आदमियों को, स्वस्थ व्यक्तियों को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा हो पाऊँगा या नहीं। अब मुझे अपनी इस शारीरिक स्थिति पर स्वयं कई बार क्षोभ होता है। खैर, यह सब अपने हाथ में नहीं है।
दो
जिन गुरूजी ने मुझे पढ़ाया था उनके प्रति आज
भी मेरी श्रद्धा है। मैं
विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से भी उनके गाँव गया था। बीच-बीच में वे भी
मुझसे मिलते रहते हैं। श्री कीर्तिराम गुरूजी बहुत ही सज्जन थे, अब उनका
देहावसान हो चुका है। मुझे स्मरण है कि उस स्कूल के चौकीदार का नाम
भगेलाराम साहू था। उनका लड़का गरीबाराम साहू मेरी कक्षा में ही पढ़ता था।
श्री भगेलगाराम की भी बाद में मृत्यु हो गई। उनका लड़का शिक्षकीय कार्य
में आकर, वहीं के स्कूल में प्रधान अध्यापक बनने के बाद सेवानिवृत्त हो
गया। जब मैं सन् 1960 में जिला शिक्षक संघ का अध्यक्ष हुआ तब गरीबाराम
साहू का भी उसमें अच्छा योगदान था। उस स्कूल में नवागाँव, खटोलिया, खटोला,
सकेरी डोमनपुर, भीमपुरी, जूनापारा, कंचनपुर, बाजार सिंघनपुरी, खोबरा,
नेवसा, चुरहा आदि आठ-दस गाँव के लड़के पढ़ने आते थे। इन लड़कों में बहुतों
से अच्छी तरह जुड़ गया था। जीवनसिंह छीपा, उधोराम यादव, कुछ कुर्मी परिवार
के लड़के, गुमानसिंह गोंड़ आदि बहुत से लोग हैं, जिनकी स्मृतियाँ आज भी
हैं। मुझे अपनी उस अवस्था में गुल्ली-डंडा खेलने व पत्थर मारकर पेड़ से फल
गिराना कभी न आ सका, इसका मेरे मन में बड़ा रंज रहता था। मैं दूसरे लड़कों
को बड़ी हसरत की नजर से देखता था। किंतु दौड़ लगाने, पानी में तैरने, पेड़
पर चढ़ने, घोड़े की सवारी करने में जरूर तेज था। बाल्यावस्था और कॉलेज के
दूसरे वर्ष तक मैं दुबला-पतला था, किंतु कबड्डी के खेल में या कुश्ती आदि
में अपने से बड़े लोगों को भी परास्त कर देता था। बाद में मैट्रिक और
कॉलेज की शिक्षा के समय हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित मंदिर के एक अहाते
में दंड-बैठक, मुगदल भाँजना आदि कार्य किया करता था। गरमी के दिनों में
शाम को सिंघनपुरी गाँव के अंतिम छोर पर पूर्व दिशा में ग्राम खटोलिया के
तालाब में, जो हम लोगों का ही था, घंटों नहाते थे। तालाब के भीतर
आँख-मिचौली का भी खेल खेलते थे।
पानी में डूबकर भीतर-ही-भीतर जाना, यह बड़ा पुराना खेल माना जाता था। उस तालाब के पास एक गूलर, एक इमली और अकोल का वृक्ष था। लोग कहते थे कि वहाँ भूत का निवास है। ये भूत उस तालाब में आ जाते हैं और छोटे बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं। इसका उस समय हम लोगों को भय लगा रहता था। कभी-कभी रास्ते में या किसी स्थान पर देर होने पर खास तौर से बरसात के दिनों में, पीपल या बरगद के वृक्षों पर बहुत से जुगनुओं का समूह होता था, जो ऊपर से पूरे वृक्ष को घेर लेते थे। सन्नाटे की अजीब सी आवाज आती थी। उस समय निश्चित रूप से हम लोगों को भूत का भय हो जाता था। हमारे पीछे चलनेवाले नौकर, जो अकसर टीकाराम पंडित हुआ करता था, से जानबूझकर हम जोर-जोर से बाते करने लगते थे। बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते थे। लेकिन जैसे ही वृक्ष के नीचे से बाहर निकल आते थे, हम साहसी हो जाते थे। आज उन सब स्थितियों का स्मरण करने में आनंद आता है। गाँव की जिंदगी की स्वाभाविकता मन में डूब सी जाती है। हमारे गाँव के पास ही, सीमा के भीतर ही घोघरा गाँव में एक फुलवारी नाला बहता है। उसके दूसरी तरफ भगवान् राम का मंदिर था। वहाँ एक अच्छा बगीचा था; लेकिन यह स्थान पूर्ण रूपेण निर्जन था। अब तो हरे वृक्ष कट गए हैं, लेकिन उस समय घने वृक्ष थे। साजा, महुआ, सेमर के झाड़ काफी तादात में थे। सिंघनपुरी की पश्चिम दिशा में बाजार से गुजरकर, नाले में उतरकर, फिर चढ़ाव चढ़कर तीन फर्लांग जाने पर यह स्थान मिलता था। बीच में मुसलमानों का कब्रिस्तान था। वहीं नाले के कारण गहरा उतार-चढ़ाव था। मैं लगातार कॉलेज जीवन और पढ़ाई की समाप्ति तक इस रास्ते में उस निर्जन स्थान पर जाता हूँ जिसे ‘चितावर’ कहते थे। वह बड़ा मनोरम स्थान था।
कब्रिस्तान के ऊपरी छोर पर बरगद का एक पुराना वृक्ष था। उस पर गाहे-बगाहे चील, कौए, कई प्रकार के पंछी और अजगर का डेरा था। कभी-कभी उल्लू के बोलने की आवाज आती थी, जो बड़ी भयावह मालूम पड़ती थी। इस प्रकार की धारणा बनी थी कि जब उल्लू बोलता है तो कोई-न-कोई मरता है, इसलिए मन में दहशत होती थी। बरगद से पार होने के बाद चितावर में एक बहुत बड़ा पत्थर था। उसके आधे भाग में पानी रहता था और आधे हिस्से में पैर फैलाकर बैठ सकते थे। मैं उस पर घंटों बैठा करता था। अधिकांश कविताएँ वहीं बैठ कर लिखीं। स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज के दिनों तक मैंने बहुत सी कविताएँ, कहानियाँ लिखीं। उनमें से कुछ तो मकान परिवर्तन के कारण गुम हो गईं। उसके बाद भी कुछ बचा है। उस कब्रिस्तान से गुजरने के बाद मुझे कभी कोई जिन्न या भूत दिखाई नहीं पड़ा। धीरे-धीरे साहस बढ़ने पर रात को भी उधर से निकल जाता था। बचपन में मैंने गाँव की महिलाओं को तथाकथित भूत पकड़े हुए भी देखा है। एक तो सोनू छीपा की घरवाली थी। वह कहीं खार की तरफ गई थी। ‘खार’ बहुत से खेतों के समूह को कहते हैं। वहाँ से लौटने के बाद उसे भूत ने पकड़ लिया। भूत भगाने के लिए जूट की रस्सी बनाकर उसे मारना, धूनी लगाना आदि सारे कार्य किए गए। उसे देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। मैं भी पीछे से देखता। इस पर पिताजी की डाँट भी पड़ती थी। कभी-कभी तो दो-तीन तमाचे भी लग जाते थे। वे कहते थे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भागो ! इसी प्रकार एक बार पं. हरदेवलालजी की लड़की को भी तथाकथित भूत ने पकड़ लिया। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि वास्तव में कोई भूत है या नहीं। बाद में मैंने इस प्रकार की कल्पना की, संभवतः जिन महिलाओं को हिस्टीरिया की बीमारी हो जाती है, वे उन्माद अवस्था में कुछ अनाप-शनाप बोलती हैं या हरकत करती हैं, उसको भूत पकड़ना कहते हैं। मैंने कभी अपनी जिंदगी में न कभी भूत देखा, और न ही आज तक किसी भूत ने मुझे आज तक सताया।
साँप काटने की भी दो-चार घटनाएँ हुईं। साँप काटे हुए व्यक्ति को मैंने अपने सामने देखा। उसके ऊपर पानी डालना, नीम की पत्ती खिलाना, रस्सी के टुकड़ों तथा धोती से बाँधना, झाड़ना, फूँकना, छुरी से चीरा लगाना-यह सब होता था। मैंने यह भी देखा कि हमारे पिताजी एक थाली में कुछ लगाकर, जिसको भूत लगता था उसकी पीठ पर फेंकते थे। मैंने जिन व्यक्तियों को साँप काटे हुए देखा, उनमें से अनेक तो बच गए। अब चाहे वे झाड़-फूँक से या साँप के जहरीले न होने की वजह से बच गए हों; पर श्रेय तो झाड़-फूँक करनेवालों को ही मिलता था। मैंने कुछ ऐसे भी व्यक्तियों को देखा है, जिन्हें साँप ने काटा और उनकी झाड़-फूँक की गई उसके बाद भी वे नहीं बचे। किंतु सन् 1964 की एक घटना मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर वकील हो गया था। मैं सर्वोदय भूदान में काम कर रहा था। उस समय विनोबाजी की पैदल यात्रा बिलासपुर जिले में हो रही थी। मैं भूदान यज्ञ आंदोलन की जिला स्तरीय समिति का प्रमुख था। उस यात्रा दल के साथ मैं भी था। बिलासपुर जिले का आखिरी पड़ाव था। वहाँ से पश्चिम की ओर करीब एक सौ कि.मी. के फासले पर पांडातराई नाम का गाँव है। वहाँ विनोबाजी का प्रवचन होना था। उस दिन शाम को बरसात हो गई थी। कुछ देर में बरसात खत्म हो गई। काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी। विनोबाजी ने प्रवचन किया
पानी में डूबकर भीतर-ही-भीतर जाना, यह बड़ा पुराना खेल माना जाता था। उस तालाब के पास एक गूलर, एक इमली और अकोल का वृक्ष था। लोग कहते थे कि वहाँ भूत का निवास है। ये भूत उस तालाब में आ जाते हैं और छोटे बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं। इसका उस समय हम लोगों को भय लगा रहता था। कभी-कभी रास्ते में या किसी स्थान पर देर होने पर खास तौर से बरसात के दिनों में, पीपल या बरगद के वृक्षों पर बहुत से जुगनुओं का समूह होता था, जो ऊपर से पूरे वृक्ष को घेर लेते थे। सन्नाटे की अजीब सी आवाज आती थी। उस समय निश्चित रूप से हम लोगों को भूत का भय हो जाता था। हमारे पीछे चलनेवाले नौकर, जो अकसर टीकाराम पंडित हुआ करता था, से जानबूझकर हम जोर-जोर से बाते करने लगते थे। बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते थे। लेकिन जैसे ही वृक्ष के नीचे से बाहर निकल आते थे, हम साहसी हो जाते थे। आज उन सब स्थितियों का स्मरण करने में आनंद आता है। गाँव की जिंदगी की स्वाभाविकता मन में डूब सी जाती है। हमारे गाँव के पास ही, सीमा के भीतर ही घोघरा गाँव में एक फुलवारी नाला बहता है। उसके दूसरी तरफ भगवान् राम का मंदिर था। वहाँ एक अच्छा बगीचा था; लेकिन यह स्थान पूर्ण रूपेण निर्जन था। अब तो हरे वृक्ष कट गए हैं, लेकिन उस समय घने वृक्ष थे। साजा, महुआ, सेमर के झाड़ काफी तादात में थे। सिंघनपुरी की पश्चिम दिशा में बाजार से गुजरकर, नाले में उतरकर, फिर चढ़ाव चढ़कर तीन फर्लांग जाने पर यह स्थान मिलता था। बीच में मुसलमानों का कब्रिस्तान था। वहीं नाले के कारण गहरा उतार-चढ़ाव था। मैं लगातार कॉलेज जीवन और पढ़ाई की समाप्ति तक इस रास्ते में उस निर्जन स्थान पर जाता हूँ जिसे ‘चितावर’ कहते थे। वह बड़ा मनोरम स्थान था।
कब्रिस्तान के ऊपरी छोर पर बरगद का एक पुराना वृक्ष था। उस पर गाहे-बगाहे चील, कौए, कई प्रकार के पंछी और अजगर का डेरा था। कभी-कभी उल्लू के बोलने की आवाज आती थी, जो बड़ी भयावह मालूम पड़ती थी। इस प्रकार की धारणा बनी थी कि जब उल्लू बोलता है तो कोई-न-कोई मरता है, इसलिए मन में दहशत होती थी। बरगद से पार होने के बाद चितावर में एक बहुत बड़ा पत्थर था। उसके आधे भाग में पानी रहता था और आधे हिस्से में पैर फैलाकर बैठ सकते थे। मैं उस पर घंटों बैठा करता था। अधिकांश कविताएँ वहीं बैठ कर लिखीं। स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज के दिनों तक मैंने बहुत सी कविताएँ, कहानियाँ लिखीं। उनमें से कुछ तो मकान परिवर्तन के कारण गुम हो गईं। उसके बाद भी कुछ बचा है। उस कब्रिस्तान से गुजरने के बाद मुझे कभी कोई जिन्न या भूत दिखाई नहीं पड़ा। धीरे-धीरे साहस बढ़ने पर रात को भी उधर से निकल जाता था। बचपन में मैंने गाँव की महिलाओं को तथाकथित भूत पकड़े हुए भी देखा है। एक तो सोनू छीपा की घरवाली थी। वह कहीं खार की तरफ गई थी। ‘खार’ बहुत से खेतों के समूह को कहते हैं। वहाँ से लौटने के बाद उसे भूत ने पकड़ लिया। भूत भगाने के लिए जूट की रस्सी बनाकर उसे मारना, धूनी लगाना आदि सारे कार्य किए गए। उसे देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। मैं भी पीछे से देखता। इस पर पिताजी की डाँट भी पड़ती थी। कभी-कभी तो दो-तीन तमाचे भी लग जाते थे। वे कहते थे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भागो ! इसी प्रकार एक बार पं. हरदेवलालजी की लड़की को भी तथाकथित भूत ने पकड़ लिया। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि वास्तव में कोई भूत है या नहीं। बाद में मैंने इस प्रकार की कल्पना की, संभवतः जिन महिलाओं को हिस्टीरिया की बीमारी हो जाती है, वे उन्माद अवस्था में कुछ अनाप-शनाप बोलती हैं या हरकत करती हैं, उसको भूत पकड़ना कहते हैं। मैंने कभी अपनी जिंदगी में न कभी भूत देखा, और न ही आज तक किसी भूत ने मुझे आज तक सताया।
साँप काटने की भी दो-चार घटनाएँ हुईं। साँप काटे हुए व्यक्ति को मैंने अपने सामने देखा। उसके ऊपर पानी डालना, नीम की पत्ती खिलाना, रस्सी के टुकड़ों तथा धोती से बाँधना, झाड़ना, फूँकना, छुरी से चीरा लगाना-यह सब होता था। मैंने यह भी देखा कि हमारे पिताजी एक थाली में कुछ लगाकर, जिसको भूत लगता था उसकी पीठ पर फेंकते थे। मैंने जिन व्यक्तियों को साँप काटे हुए देखा, उनमें से अनेक तो बच गए। अब चाहे वे झाड़-फूँक से या साँप के जहरीले न होने की वजह से बच गए हों; पर श्रेय तो झाड़-फूँक करनेवालों को ही मिलता था। मैंने कुछ ऐसे भी व्यक्तियों को देखा है, जिन्हें साँप ने काटा और उनकी झाड़-फूँक की गई उसके बाद भी वे नहीं बचे। किंतु सन् 1964 की एक घटना मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर वकील हो गया था। मैं सर्वोदय भूदान में काम कर रहा था। उस समय विनोबाजी की पैदल यात्रा बिलासपुर जिले में हो रही थी। मैं भूदान यज्ञ आंदोलन की जिला स्तरीय समिति का प्रमुख था। उस यात्रा दल के साथ मैं भी था। बिलासपुर जिले का आखिरी पड़ाव था। वहाँ से पश्चिम की ओर करीब एक सौ कि.मी. के फासले पर पांडातराई नाम का गाँव है। वहाँ विनोबाजी का प्रवचन होना था। उस दिन शाम को बरसात हो गई थी। कुछ देर में बरसात खत्म हो गई। काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी। विनोबाजी ने प्रवचन किया
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i